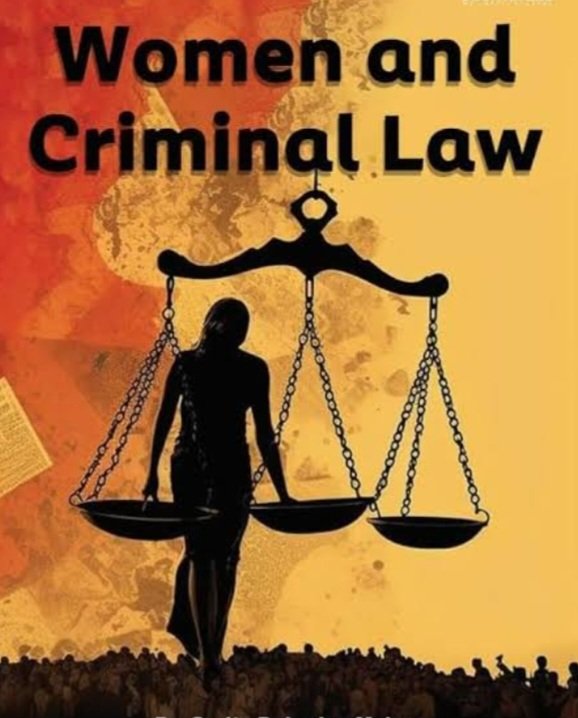अध्याय 1: महिलाओं के खिलाफ हिंसा: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ
1. महिलाओं के खिलाफ हिंसा (VAW) की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा दी गई परिभाषा
महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Violence Against Women – VAW) को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों में परिभाषित किया गया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:
- संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (1993) के अनुसार, “महिलाओं के खिलाफ हिंसा से तात्पर्य किसी भी लिंग-आधारित हिंसा से है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न हो सकता है या होने की संभावना हो। इसमें घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, यौन शोषण, दहेज संबंधी उत्पीड़न, और अन्य हानिकारक प्रथाएँ शामिल हैं।”
- CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 1979 के तहत भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को महिला अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) महिलाओं के खिलाफ हिंसा को “शारीरिक, यौन या मानसिक हानि पहुंचाने या धमकी देने की किसी भी क्रिया” के रूप में परिभाषित करता है।
2 (a). ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाज में स्वीकार्यता कैसे मिली?
इतिहास गवाह है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कई संस्कृतियों और समाजों में वैधता प्रदान की गई थी। प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता था, जिसके कारण घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और सम्मान के नाम पर हत्या जैसी प्रथाएँ विकसित हुईं।
- कई देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता था।
- महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया, जिससे वे आर्थिक रूप से निर्भर हो गईं।
- मध्यकालीन कानूनों में महिलाओं को पति की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य किया गया था।
- कई संस्कृतियों में विधवा प्रथा, सती प्रथा और ऑनर किलिंग को सामाजिक रूप से स्वीकृति मिली।
हालांकि, आधुनिक मानवाधिकार आंदोलनों और नारीवादी आंदोलनों के कारण यह दृष्टिकोण बदला है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं।
2 (b). विभिन्न विवाह कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए कितने उत्तरदायी हैं?
विभिन्न देशों में प्रचलित विवाह कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
- बाल विवाह: कई देशों में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं।
- दहेज प्रथा: भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में दहेज के कारण महिलाओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।
- बहुविवाह (Polygamy): कुछ देशों में पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति दी गई है, जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है।
- विवाह के भीतर बलात्कार (Marital Rape): कई देशों में इसे अपराध नहीं माना जाता, जिससे पति अपनी पत्नी के खिलाफ यौन हिंसा कर सकते हैं।
- तलाक कानूनों में भेदभाव: कई देशों में तलाक की प्रक्रिया महिलाओं के लिए कठिन होती है, जिससे वे हिंसा झेलने के लिए विवश होती हैं।
3. महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहल
कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं:
- CEDAW (1979): महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए यह संधि बनाई गई।
- संयुक्त राष्ट्र की 1993 की घोषणा: इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकार हनन के रूप में स्वीकार किया गया।
- बीजिंग डिक्लेरेशन (1995): महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से यह घोषणापत्र अपनाया गया।
- Istanbul Convention (2011): यह यूरोप में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण संधि है।
अध्याय 2: संयुक्त राष्ट्र का 1993 का महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन घोषणा पत्र
1. 1993 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा और इसमें महिलाओं के अधिकारों की परिभाषा
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को अपनाई गई “महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा” (Declaration on the Elimination of Violence Against Women) में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।
- इस घोषणा के तहत शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा को महिलाओं के खिलाफ अपराध माना गया।
- इसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन दासता, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना, और युद्धकालीन यौन हिंसा को शामिल किया गया।
- इस घोषणा में महिलाओं के समान अधिकार, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी दी गई।
हालांकि, इस घोषणा के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ आईं, जैसे कि कुछ देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को अभी भी वैध माना जाता है, और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएँ हैं।
2. इस अलग घोषणा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
- CEDAW (1979) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था।
- कई देशों में घरेलू हिंसा और यौन अपराधों को निजी मामला माना जाता था।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता थी।
3. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारियाँ
संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा के तहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ डाली गईं:
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों को लागू करना।
- पीड़ितों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करना।
- महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कदम उठाना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानसिकता परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
अध्याय 3: महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध
1. महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समाज पर प्रभाव
महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है:
- इससे महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है।
- आर्थिक रूप से भी समाज प्रभावित होता है, क्योंकि हिंसा के कारण उत्पादकता और श्रम शक्ति कम होती है।
2. महिलाओं के जीवन चक्र में विभिन्न प्रकार की हिंसा
महिलाओं को जीवन भर अलग-अलग प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है:
- बाल्यावस्था: कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, यौन शोषण।
- युवा अवस्था: दहेज प्रथा, बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न।
- वृद्धावस्था: संपत्ति से वंचित करना, दुर्व्यवहार।
3. विभिन्न प्रकार की हिंसा
- शारीरिक हिंसा: मारपीट, तेजाब हमला।
- यौन हिंसा: बलात्कार, मानव तस्करी।
- मानसिक हिंसा: धमकी, भावनात्मक शोषण।
- आर्थिक हिंसा: संपत्ति के अधिकार से वंचित करना।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त कानून और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।
आपके अनुरोध के अनुसार, सभी प्रश्नों और उत्तरों को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है।
महिलाओं के विरुद्ध वैश्विक अपराधों पर एक टिप्पणी
(i) बलात्कार (Rape)
बलात्कार महिलाओं के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है, जिसमें उनकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। यह न केवल उनके शरीर बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है।
(ii) बलात्कार पीड़िता के खिलाफ हिंसा (Violence Against Rape Victims)
कई बार बलात्कार पीड़िताओं को समाज द्वारा तिरस्कार, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। न्याय की मांग करने पर उन्हें बदनाम किया जाता है।
(iii) वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)
जब किसी पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। कई देशों में इसे अब भी अपराध नहीं माना जाता।
(iv) घरेलू हिंसा (Domestic Violence)
पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा महिलाओं पर किए गए शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हमले को घरेलू हिंसा कहते हैं।
(v) ऑनर किलिंग (Honor Killings)
जब परिवार की ‘इज्जत’ के नाम पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, तो इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। यह अपराध अधिकतर विवाह और रिश्तों से जुड़ा होता है।
(vi) दहेज हत्या (Dowry Violence)
दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करना, उन्हें जलाना या मार डालना दहेज हिंसा का हिस्सा है।
(vii) एसिड अटैक (Acid Throwing)
महिलाओं पर तेजाब फेंककर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना एक जघन्य अपराध है, जो बदला या अस्वीकृत प्रेम के कारण किया जाता है।
(viii) जबरन विवाह (Forced Marriage)
बिना महिला की सहमति के उसे विवाह के लिए बाध्य करना एक अमानवीय अपराध है।
(ix) जबरन मोटा करना (Force-Feeding)
कुछ समाजों में महिलाओं को आकर्षक बनाने के लिए जबरन अधिक खिलाया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
(x) भीड़ द्वारा हिंसा (Mob Violence)
कई बार महिलाओं को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से मारपीट या हमला।
(xi) पीछा करना (Stalking)
महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करना, उसे धमकाना या डराना एक गंभीर अपराध है।
(xii) यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)
कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानों और घरों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
(xiii) मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति (Human Trafficking and Forced Prostitution)
महिलाओं और बच्चियों को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए बेचा और खरीदा जाता है।
(xiv) विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार (Mistreatment of Widows)
कुछ समाजों में विधवाओं को अपशगुन माना जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है।
(xv) जादू-टोना का आरोप (Accusations of Witchcraft)
कई देशों में महिलाओं को जादूगरनी बताकर पीटा या मार दिया जाता है।
(xvi) राज्य द्वारा हिंसा (State Violence)
युद्ध के समय महिलाओं के साथ बलात्कार और उन्हें यौन दासता में झोंक देना एक युद्ध अपराध है।
(xvii) जबरन नसबंदी और गर्भपात (Forced Sterilization and Forced Abortion)
कुछ सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर महिलाओं को जबरन नसबंदी और गर्भपात के लिए मजबूर करती हैं।
(xviii) पुलिस और अधिकारियों द्वारा हिंसा (Violence by Police and Authorities)
कई बार पुलिस और सरकारी अधिकारी महिलाओं का यौन शोषण या हिंसा करते हैं।
(xix) पत्थर मारकर हत्या और कोड़े लगाना (Stoning and Flogging)
कुछ देशों में महिलाओं को पत्थर मारकर हत्या करने या कोड़े मारने जैसी सजाएं दी जाती हैं।
(xx) महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation)
कुछ समुदायों में परंपरा के नाम पर महिलाओं के जननांगों को विकृत किया जाता है।
(xxi) स्तन दबाना (Breast Ironing)
कुछ अफ्रीकी देशों में लड़कियों के स्तनों को दबाकर उनके विकास को रोकने की कोशिश की जाती है।
(xxii) प्रसूति हिंसा (Obstetric Violence)
गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पतालों में अमानवीय व्यवहार किया जाता है।
(xxiii) खेल संबंधी हिंसा (Sport-Related Violence)
महिला खिलाड़ियों को खेल जगत में यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है।
अध्याय 4
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए सक्रिय आंदोलन
1. वैश्विक स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए किए गए प्रयास
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलन और संगठन काम कर रहे हैं, जैसे:
- संयुक्त राष्ट्र का CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- “Me Too” और “Times Up” जैसे अभियान
- यौन हिंसा विरोधी कानूनों का निर्माण और संशोधन
- घरेलू हिंसा और दहेज हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून
2. महिलाओं को न्याय पाने में आने वाली चुनौतियाँ
- न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता और लंबा समय लगना
- सामाजिक दबाव और बदनामी का डर
- पुलिस और न्याय प्रणाली में संवेदनशीलता की कमी
भाग II
अध्याय 5: सती प्रथा का उन्मूलन
1. सती (निवारण) अधिनियम, 1987 क्यों पारित किया गया?
यह कानून सती प्रथा को रोकने के लिए पारित किया गया था, जिसमें विधवाओं को उनके पति की चिता में जबरन जलाया जाता था।
2. परिभाषाएँ
(i) महिमामंडन (Glorification) – सती को महिमामंडित करने वाले कृत्य, जैसे मंदिर बनाना या महोत्सव आयोजित करना।
(ii) सती (Sati) – किसी महिला को पति की मृत्यु के बाद जलाकर मार डालना।
(iii) मंदिर (Temple) – वह स्थान जहाँ सती का पूजन किया जाता है।
3. सती में सहायक कृत्य कौन से हैं?
जो कोई सती को उकसाता, सहमति देता या उसमें मदद करता है, वह दोषी माना जाएगा।
4. क्या सती का महिमामंडन भी दंडनीय है?
हाँ, सती का समर्थन, प्रचार या महिमामंडन करना भी अपराध है।
अध्याय 6: दहेज निषेध
1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 क्यों आवश्यक था?
दहेज के कारण महिलाओं की हत्या और उत्पीड़न बढ़ रहे थे, इसलिए यह कानून लागू किया गया।
2. दहेज की परिभाषा और दंड
- दहेज (Dower) – विवाह के समय वर-पक्ष द्वारा वधू-पक्ष से धन या वस्तुएं लेना।
- दंड – दहेज लेने या देने पर 5 साल की जेल और जुर्माना।
अध्याय 6: दहेज निषेध
3. (i) विज्ञापन पर प्रतिबंध
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4ए के तहत, किसी भी प्रकार के दहेज के संबंध में विज्ञापन देना प्रतिबंधित है। इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दहेज की पेशकश, मांग, या स्वीकार करने का विज्ञापन शामिल है। इस प्रकार का विज्ञापन करने पर दंडस्वरूप 6 महीने तक की कारावास या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
(ii) दहेज देने या लेने के लिए समझौता
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत, किसी भी व्यक्ति के बीच दहेज देने या लेने के लिए कोई समझौता अवैध और अमान्य होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह में दहेज प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को रोकना है।
4. दहेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसे महिला को हस्तांतरित करना होगा
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, यदि विवाह के समय किसी महिला के नाम पर या उसके विवाह से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दहेज प्राप्त किया जाता है, तो वह दहेज उस महिला को हस्तांतरित करना आवश्यक है।
यदि महिला नाबालिग है, तो उसे विवाह के दो साल के भीतर या उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद छह महीने के भीतर उसे सौंपा जाना चाहिए। यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दहेज उसके बच्चों को और यदि संतान नहीं है तो उसके माता-पिता को सौंपा जाएगा।
यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो दोषी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने से 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
5. (i) अपराधों का संज्ञान (Cognizance of Offences)
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) हैं। इसका अर्थ यह है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और मुकदमा केवल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जा सकता है।
(ii) सबूत का बोझ (Burden of Proof)
इस अधिनियम के तहत आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त (Accused) की होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति पर दहेज लेने या देने का आरोप लगाया जाता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया। यह प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लागू किया गया है।
(iii) दहेज निषेध अधिकारी (Dowry Prohibition Officers)
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8बी के तहत सरकार दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ये अधिकारी दहेज संबंधी अपराधों की जांच करते हैं, मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
अध्याय 7: अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
1. अधिनियम के उद्देश्य और दायरा
इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और वेश्यावृत्ति के अवैध धंधे को समाप्त करना था। यह अधिनियम वेश्यालयों को बंद करने, दलालों और तस्करों को दंडित करने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बनाए गए प्रावधानों को लागू करता है।
1978 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन:
- सजा को कड़ा किया गया – दोषियों को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है।
- 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने पर कड़ी सजा – कम से कम 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।
- पुनर्वास केंद्रों की स्थापना – पीड़ितों को संरक्षण गृह में रखा जाता है।
2. परिभाषाएँ
(i) वेश्यालय (Brothel): वह स्थान जहाँ किसी भी रूप में वेश्यावृत्ति होती है या उससे संबंधित गतिविधियाँ संचालित होती हैं।
(ii) बच्चा (Child): अधिनियम के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है।
(iii) सुधारात्मक संस्था (Corrective Institution): ऐसा केंद्र जहाँ पीड़ितों को पुनर्वास और सुधार के लिए रखा जाता है।
(iv) वेश्यावृत्ति (Prostitution): किसी महिला या व्यक्ति द्वारा वित्तीय लाभ के लिए यौन गतिविधि करना।
(v) संरक्षण गृह (Protective Home): वह स्थान जहाँ वेश्यावृत्ति से बचाए गए व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जाता है।
3. वेश्यालय संचालन में संलिप्त व्यक्तियों के लिए दंड
धारा 3 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने देता है, संचालित करता है, या प्रबंध करता है, तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
यदि यह अपराध दोहराया जाता है, तो सजा न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की होगी।
4. वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने के लिए दंड
धारा 4 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की वेश्यावृत्ति से अर्जित आय पर निर्भर करता है, तो उसे 2 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है।
5. किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना या ले जाना
धारा 5 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को वेश्यावृत्ति में धकेलता है, बहकाता है, या उसे इसके लिए ले जाता है, तो उसे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु का है, तो सजा 7 साल से आजीवन कारावास तक हो सकती है।
6. वेश्यावृत्ति के परिसर में किसी व्यक्ति को जबरन रोकना
धारा 6 के तहत, यदि कोई किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए जबरन किसी परिसर में रोकता है, तो उसे 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
7. सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति के लिए दंड
धारा 7 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करता है, तो उसे 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
8. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर टिप्पणी
(i) वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बहकाना या प्रलोभन देना:
यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बहकाता है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
(ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए बहकाना:
यदि पुलिस हिरासत या अन्य सुरक्षा स्थान पर कोई व्यक्ति किसी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है, तो उसे 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।
(iii) सुधारात्मक संस्था में हिरासत:
वेश्यावृत्ति से बचाए गए व्यक्तियों को सुधार गृह में पुनर्वास के लिए भेजा जा सकता है।
(iv) वेश्यालयों से व्यक्तियों को छुड़ाना:
पुलिस को अधिकार है कि वे किसी महिला को वेश्यालय से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर भेजे।
(v) वेश्यालय से निकाले गए या बचाए गए व्यक्तियों की मध्यवर्ती हिरासत:
इन व्यक्तियों को पुनर्वास केंद्रों में रखा जा सकता है।
(vi) किसी स्थान से वेश्याओं को हटाना:
स्थानीय प्रशासन को अधिकार है कि वे किसी क्षेत्र से वेश्यावृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई करें।
9. दोषी व्यक्तियों की सूचना का प्रावधान
धारा 11 के अनुसार, पहले से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अपना पता पुलिस को बताना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर उसे 6 महीने तक की कैद हो सकती है।
अध्याय 7: अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
10. बिना वारंट तलाशी के दौरान पालन की जाने वाली दिशानिर्देश (धारा 15)
धारा 15 के तहत, पुलिस अधिकारी को बिना वारंट तलाशी लेने से पहले निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है:
- विशेष पुलिस अधिकारी (Special Police Officer) द्वारा तलाशी: तलाशी केवल पुलिस के विशेष अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
- महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति: यदि किसी परिसर में महिलाओं की उपस्थिति संदिग्ध है, तो तलाशी के दौरान महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य जिम्मेदार महिला को उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- तलाशी के दौरान महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार: तलाशी प्रक्रिया में शामिल महिलाओं के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट को सूचना देना: तलाशी के बाद, जब्त वस्तुओं और बचाए गए व्यक्तियों की जानकारी तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए।
- अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति: यदि तलाशी के दौरान कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
11. बचाए गए व्यक्तियों को माता-पिता या अभिभावकों को सौंपने से पहले पालन की जाने वाली शर्तें
अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत, किसी व्यक्ति को माता-पिता या अभिभावक को सौंपने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है:
- मजिस्ट्रेट की अनुमति: बचाए गए व्यक्ति को केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही माता-पिता या अभिभावकों को सौंपा जा सकता है।
- अभिभावकों की पृष्ठभूमि की जांच: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि माता-पिता या अभिभावक स्वयं अवैध व्यापार में शामिल न हों।
- बचाए गए व्यक्ति की इच्छा: यदि बचाया गया व्यक्ति अपनी इच्छा से माता-पिता के पास नहीं जाना चाहता, तो उसे संरक्षण गृह में रखा जा सकता है।
- सुरक्षित वातावरण की गारंटी: यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिले।
12. वेश्यालय बंद करने और अपराधियों को परिसर से बेदखल करने का आदेश कब दिया जा सकता है?
धारा 18 के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह किसी परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश दे और अपराधियों को वहां से बेदखल कर दे।
ऐसा आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जा सकता है:
- यदि कोई स्थान बार-बार अनैतिक व्यापार में लिप्त पाया जाता है।
- यदि परिसर का मालिक या प्रबंधक इसे वेश्यावृत्ति के लिए किराए पर देता है।
- यदि पुलिस की जांच में पुष्टि हो जाए कि वहां अनैतिक व्यापार हो रहा है।
- यदि बचाए गए व्यक्ति की सुरक्षा के लिए परिसर को बंद करना आवश्यक हो।
13. अधिनियम में संरक्षण गृहों और सुधारात्मक संस्थाओं के लिए प्रावधान
इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा संरक्षण गृह (Protective Homes) और सुधारात्मक संस्थाएं (Corrective Institutions) स्थापित की जाती हैं, जहां पीड़ितों को पुनर्वास और सुधार की सुविधाएं मिलती हैं।
- संरक्षण गृह: इसमें पीड़ितों को अस्थायी रूप से रखा जाता है, जहां वे कानूनी और मानसिक सहायता प्राप्त करते हैं।
- सुधारात्मक संस्थाएं: यहां पीड़ितों को शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल दिए जाते हैं ताकि वे समाज में पुनः आत्मनिर्भर बन सकें।
- निगरानी और देखभाल: इन संस्थानों में रखे गए व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाती है।
अध्याय 8: महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का निषेध
1. अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम, 1986 के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं
इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना और उनके अश्लील चित्रण (Indecent Representation) को रोकना है। इसके तहत किसी भी प्रकार की सामग्री, जो महिलाओं की छवि को अश्लील रूप में प्रस्तुत करती है, को प्रतिबंधित किया गया है।
मुख्य विशेषताएं:
- अश्लील विज्ञापनों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, फिल्मों, पोस्टरों, पेंटिंग, डिजिटल माध्यमों आदि पर प्रतिबंध।
- कानून का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान।
- पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने और सामग्री जब्त करने का अधिकार।
2. परिभाषाएँ
(i) विज्ञापन (Advertisement): किसी उत्पाद, सेवा, या विचार के प्रचार हेतु किए गए दृश्य, लिखित, या ऑडियो संचार को विज्ञापन कहते हैं।
(ii) अश्लील प्रतिनिधित्व (Indecent Representation): महिलाओं के शरीर या उनकी छवि को कामुक, अश्लील या अनैतिक तरीके से प्रस्तुत करना।
3. कौन से कार्य अपराध माने जाते हैं और अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं?
- महिलाओं को कामुक और अश्लील रूप में चित्रित करने वाली किताबें, पोस्टर, सिनेमा, और डिजिटल सामग्री।
- महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन और प्रकाशन।
- इंटरनेट, सोशल मीडिया, या अन्य डिजिटल माध्यमों पर महिलाओं की अश्लील छवियों का प्रसार।
अध्याय 9: गर्भपात (Termination of Pregnancy)
1. चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 क्यों बनाया गया? यह किन आधारों पर गर्भपात की अनुमति देता है?
यह अधिनियम महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है और अवैध गर्भपात को रोकता है।
गर्भपात के आधार:
- यदि गर्भ जारी रखने से महिला का जीवन खतरे में हो।
- यदि भ्रूण में गंभीर विकृति हो।
- यदि गर्भधारण बलात्कार या अन्य आपराधिक कृत्य का परिणाम हो।
- यदि गर्भावस्था महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
अध्याय 10: कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide)
1. कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ और 1994 के अधिनियम के उद्देश्य
कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide) का अर्थ गर्भ में ही लड़की के भ्रूण को मार देना है। इसे रोकने के लिए सरकार ने पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 लागू किया।
अधिनियम का उद्देश्य:
- लिंग आधारित गर्भपात को रोकना।
- भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना।
- दोषियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान।
2002 के संशोधन:
- अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य।
- अवैध लिंग परीक्षण करने वालों के लिए कठोर सजा।
- लिंग चयन विज्ञापन पर प्रतिबंध।
2. परिभाषाएँ
(i) Conceptus: गर्भधारण के तुरंत बाद भ्रूण का प्रारंभिक विकास।
(ii) Embryo: निषेचन के बाद विकसित होने वाला पहला चरण।
(iii) Foetus: गर्भावस्था के आठवें सप्ताह के बाद विकसित भ्रूण।
(iv) Genetic Clinic: वह केंद्र जहां आनुवंशिक परीक्षण किए जाते हैं।
(v) Medical Geneticist: आनुवंशिक बीमारियों के विशेषज्ञ।
(vi) Pre-natal Diagnostic Procedure: गर्भ में भ्रूण की जांच की प्रक्रिया।
(vii) Pre-natal Diagnostic Techniques: भ्रूण की लिंग पहचान करने की तकनीक।
(viii) Pre-natal Diagnostic Test: गर्भ में भ्रूण का परीक्षण।
(ix) Sex Selection: लिंग आधारित भ्रूण चयन।
(x) Sonologist: अल्ट्रासाउंड करने वाला विशेषज्ञ।
अध्याय 10: कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide)
3. अधिनियम द्वारा लिंग चयन पर रोक लगाने के प्रावधान
पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीक (नियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 में लिंग चयन पर रोक लगाने के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं:
- गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण निषिद्ध: कोई भी व्यक्ति, अस्पताल, या लैब गर्भधारण से पहले या बाद में भ्रूण के लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता।
- अवैध लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध: अल्ट्रासाउंड या अन्य नैदानिक तकनीकों का उपयोग केवल चिकित्सा कारणों से किया जा सकता है, लिंग पहचान के लिए नहीं।
- डॉक्टरों पर कड़ी निगरानी: सोनोग्राफी और नैदानिक केंद्रों को सरकार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
- कठोर दंड: अधिनियम के उल्लंघन पर तीन से पांच साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
4. पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीकों के विनियमन के लिए अधिनियम में प्रावधान
- पूर्व-गर्भाधान तकनीकों का दुरुपयोग रोकना: सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
- नैदानिक प्रक्रियाओं की सख्त निगरानी: केवल चिकित्सा कारणों से ही पूर्व-प्रसव नैदानिक परीक्षण किए जा सकते हैं।
- महिला की लिखित सहमति: किसी भी पूर्व-प्रसव नैदानिक परीक्षण के लिए गर्भवती महिला की लिखित सहमति अनिवार्य है।
- दस्तावेजों का संधारण: सभी नैदानिक प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, जिससे जांच और निगरानी में सहायता मिल सके।
5. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी:
(i) पूर्व-प्रसव नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए गर्भवती महिला की लिखित सहमति:
- किसी भी नैदानिक परीक्षण से पहले गर्भवती महिला की लिखित सहमति आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महिला जबरदस्ती लिंग परीक्षण के लिए बाध्य न की जाए।
- सहमति फॉर्म पर डॉक्टर और गर्भवती महिला के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
(ii) भ्रूण के लिंग की जानकारी देने पर प्रतिबंध:
- डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, या कोई भी व्यक्ति भ्रूण के लिंग की जानकारी किसी को नहीं दे सकता।
- ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
(iii) लिंग निर्धारण की मनाही:
- यह अधिनियम किसी भी प्रकार की तकनीक या प्रक्रिया से भ्रूण का लिंग पहचानने की मनाही करता है।
- अल्ट्रासाउंड मशीन का दुरुपयोग करने पर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
6. आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लीनिकों के पंजीकरण के लिए अधिनियम में प्रावधान
- सभी आनुवंशिक केंद्रों को सरकार के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- पंजीकरण प्राप्त करने के लिए केंद्रों को सख्त नियमों का पालन करना होगा।
- सरकार को इन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और गैर-कानूनी गतिविधियों की जांच करने का अधिकार है।
7. संशोधित धारा 22 के तहत लिंग निर्धारण से जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध और दंड
- अखबारों, टेलीविजन, इंटरनेट, या किसी भी माध्यम से लिंग परीक्षण और लिंग चयन के विज्ञापन देना अपराध है।
- ऐसा करने वाले व्यक्तियों को तीन साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
- डॉक्टरों को ऐसे विज्ञापन देने वाले केंद्रों की रिपोर्ट सरकार को करनी होगी।
8. अधिनियम के तहत अपराध और उनकी सजा
9. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी:
(i) पूर्व-प्रसव नैदानिक तकनीकों के संचालन से संबंधित अनुमान:
- यदि कोई डॉक्टर या लैब गैर-कानूनी लिंग परीक्षण करता पाया जाता है, तो उसे दोषी माना जाएगा।
- बचाव के लिए डॉक्टर को सिद्ध करना होगा कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया।
(ii) अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा:
- यदि किसी अपराध के लिए कोई विशिष्ट सजा नहीं दी गई है, तो तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
(iii) अपराधों का संज्ञान:
- मजिस्ट्रेट ही इस अधिनियम के तहत मामलों का संज्ञान ले सकते हैं।
- पीड़ित महिलाओं के परिवार के सदस्य भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
(iv) रिकॉर्ड का रखरखाव:
- सभी नैदानिक केंद्रों को प्रत्येक परीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
- रिकॉर्ड न रखने पर केंद्र का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
(v) खोज और जब्ती की शक्ति:
- सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र पर छापा मारकर रिकॉर्ड और उपकरण जब्त कर सकती है।
अध्याय 11: महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड (IPC के तहत)
1. दहेज मृत्यु (Dowry Death)
दहेज मृत्यु का अर्थ है किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर दहेज के कारण हो जाना।
कानूनी प्रावधान:
- यदि किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है और यह प्रमाणित होता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो पति और ससुराल वालों को दोषी माना जाएगा।
- धारा 304B IPC के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
2. आत्महत्या के लिए उकसाना (Abetment of Suicide)
- यदि किसी विवाहित महिला को प्रताड़ित किया जाता है और वह आत्महत्या कर लेती है, तो पति और ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना जा सकता है।
- धारा 306 IPC के तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है।
3. गर्भपात से संबंधित अपराध (Miscarriage)
IPC की विभिन्न धाराओं के तहत गर्भपात जबरन कराने या गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है।
4. अन्य अपराधों पर टिप्पणी:
(i) बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोकना या जन्म के बाद मार देना:
- IPC की धारा 315-316 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकता है या जन्म के बाद उसकी हत्या करता है, तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।
(ii) गलत तरीके से रोकना और अवैध कैद:
- IPC की धारा 339 और 340 के तहत, किसी भी महिला को जबरन रोकना या बंधक बनाना अपराध है, जिसमें 1-7 साल की सजा हो सकती है।
निष्कर्ष:
महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। जागरूकता, कड़ी सजा और समाज में मानसिकता परिवर्तन के जरिए ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
IPC के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर संक्षिप्त टिप्पणी
(iii) तेजाब हमला (Acid Throwing) – धारा 326A और 326B
- तेजाब फेंकना एक जघन्य अपराध है, जिसमें किसी महिला को गंभीर रूप से घायल करने के लिए उसके ऊपर तेजाब डाला जाता है।
- धारा 326A: पीड़ित को स्थायी क्षति पहुंचाने पर 10 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना।
- धारा 326B: केवल तेजाब फेंकने की कोशिश करने पर 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना।
(iv) अपहरण से संबंधित अपराध (Offences relating to Kidnapping) – धारा 359-369
- धारा 363: किसी भी व्यक्ति को उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति के बिना अपहरण करना अपराध है।
- धारा 366: यदि अपहरण किसी महिला से विवाह करने या उसे बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए किया जाता है, तो 10 साल तक की सजा।
(v) नाबालिग लड़की का अपहरण (Procuration of Minor Girl) – धारा 366A
- किसी लड़की (18 वर्ष से कम) को अपहरण कर किसी भी अनैतिक उद्देश्य से ले जाना अपराध है।
- इस अपराध के लिए 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
(vi) विदेशी देश से लड़की को भारत लाना (Importing of Girl from Foreign Country) – धारा 366B
- 21 साल से कम उम्र की लड़की को भारत में अवैध उद्देश्यों के लिए लाना अपराध है।
- अपराध सिद्ध होने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।
(vii) नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या खरीदना (Selling or Buying Minor for Prostitution) – धारा 372 और 373
- धारा 372: किसी भी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध है।
- धारा 373: किसी नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना भी अपराध है।
- दोनों अपराधों की सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना है।
(viii) यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) – धारा 354A
- महिला को अनुचित रूप से छूना, गलत संकेत देना, अश्लील टिप्पणी करना या यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना अपराध है।
- सजा: 1 से 3 साल की सजा और जुर्माना।
(ix) दृष्टिपात (Voyeurism) – धारा 354C
- किसी महिला की उसकी सहमति के बिना उसकी निजी गतिविधियों की तस्वीरें या वीडियो लेना अपराध है।
- पहली बार अपराध पर 1-3 साल की सजा, पुनरावृत्ति पर 3-7 साल की सजा।
(x) पीछा करना (Stalking) – धारा 354D
- यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का जबरन पीछा करता है, उसका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है, या उसे ऑनलाइन परेशान करता है, तो यह अपराध है।
- पहली बार अपराध पर 3 साल की सजा, पुनरावृत्ति पर 5 साल की सजा।
5. महिला की मर्यादा भंग करने के उद्देश्य से हमला (Assault on Woman with Intent to Outrage Her Modesty) – धारा 354
- यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या बल प्रयोग करता है, तो यह अपराध होगा।
- सजा: 1 से 5 साल की जेल और जुर्माना।
नया प्रावधान (Criminal Law Amendment Act, 2013):
- अपराध की परिभाषा को विस्तृत किया गया और दंड को कठोर बनाया गया।
- यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग और वॉययूरिज्म को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया।
6. बलात्कार (Rape) – धारा 375 और 376 (संशोधित 2013 कानून के तहत)
परिभाषा:
- यदि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला से उसकी सहमति के बिना, या दबाव डालकर, या नशीले पदार्थ देकर, या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो इसे बलात्कार माना जाएगा।
- 2013 के संशोधन में मौखिक, डिजिटल या वस्तुओं द्वारा यौन उत्पीड़न को भी बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया।
सजा:
- 7 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना।
- यदि अपराध 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ हुआ, तो 10 साल से आजीवन कारावास।
- गैंगरेप में दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
7. जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें (Justice Verma Commission Recommendations)
- यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में सख्त दंड।
- पुलिस और न्यायपालिका में सुधार।
- पीड़िता को आर्थिक और मानसिक सहायता प्रदान करना।
- संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक समानता मानकों को अपनाना।
8. सहमति (Consent) और बलात्कार के मामलों में बचाव के रूप में इसकी वैधता
- यदि महिला स्वतंत्र इच्छा से सहमति देती है, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।
- लेकिन अगर सहमति डर, धोखे, नशीली दवाओं, या बल प्रयोग के तहत ली गई है, तो यह अमान्य मानी जाएगी।
9. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार पीड़िता की सहायता के लिए निर्देश
- पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता और सुरक्षा।
- मुआवजे की व्यवस्था।
- तेजी से न्यायिक प्रक्रिया।
- विशेष पुलिस और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
10. सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) – धारा 376D
- यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करते हैं, तो यह सामूहिक बलात्कार कहलाता है।
- सजा: कम से कम 20 साल की जेल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड।
11. बलात्कार मामलों में अभियोजन पक्ष की गवाही का महत्व
- यदि पीड़िता का बयान विश्वसनीय है, तो अदालत केवल उसी के आधार पर दोष सिद्ध कर सकती है।
- मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है।
12. अप्राकृतिक अपराध (Unnatural Offences) – धारा 377
- किसी भी व्यक्ति या जानवर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध है।
- 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास।
13. द्विविवाह (Bigamy) और व्यभिचार (Adultery)
- धारा 494: कोई भी व्यक्ति पहले पति/पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता।
- धारा 497: (अब हटाई गई) व्यभिचार को अपराध के रूप में देखा जाता था।
14. धारा 498A – महिला को क्रूरता से प्रताड़ित करना
- यदि किसी महिला को पति या ससुराल वाले मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो यह अपराध है।
- सजा: 3 साल तक की जेल और जुर्माना।
15. क्या धारा 498A और 304B परस्पर अनन्य हैं?
- धारा 498A (क्रूरता) और 304B (दहेज मृत्यु) अलग-अलग अपराध हैं, लेकिन एक साथ लागू किए जा सकते हैं।
- अगर महिला की मौत दहेज के कारण होती है, तो दोनों धाराओं के तहत मुकदमा चल सकता है।
धारा 304-B के तहत बरी व्यक्ति को धारा 498-A के तहत दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं?
यदि किसी व्यक्ति को धारा 304-B (दहेज मृत्यु) के तहत बरी कर दिया जाता है, तो उसे धारा 498-A (क्रूरता से प्रताड़ित करना) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि अभियोजन पक्ष यह साबित करे कि उसने महिला के साथ क्रूरता की थी। हालांकि, यदि चार्जशीट में धारा 498-A नहीं जोड़ी गई थी, तो उसे दोषी ठहराने के लिए अभियोजन को उचित प्रक्रिया के तहत मामला फिर से दायर करना होगा।
16. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:
(i) किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर कि यदि वह कोई कार्य नहीं करेगा तो उसे दैवीय नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा – (धारा 508, IPC)
- यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर डराने या धमकाने का प्रयास करता है कि यदि वह कोई कार्य नहीं करेगा तो उसे ईश्वर या किसी अन्य दैवीय शक्ति के कोप का शिकार होना पड़ेगा, तो यह अपराध होगा।
- सजा: 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना, या दोनों।
(ii) महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से शब्द, संकेत या कृत्य करना – (धारा 509, IPC)
- यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई आपत्तिजनक शब्द, इशारा, या कार्य करता है, तो यह अपराध होगा।
- उदाहरण: अश्लील फब्तियां कसना, गलत संकेत देना, किसी महिला का पीछा करना आदि।
- सजा: 3 साल तक की जेल और जुर्माना।
विशेष साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान (Indian Evidence Act, 1872) और महिलाओं के अधिकार
1. महिलाओं के संबंध में विशेष साक्ष्य प्रावधान
- धारा 113-A: यदि कोई विवाहित महिला विवाह के 7 वर्षों के भीतर आत्महत्या कर लेती है और यह साबित हो जाता है कि उसे पति या ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, तो यह माना जाएगा कि आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाया गया था।
- धारा 113-B: यदि कोई महिला दहेज से संबंधित कारणों से मर जाती है, तो यह माना जाएगा कि पति या ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया होगा।
- धारा 146: बलात्कार के मामलों में पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. क्या बलात्कार मामलों में पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है?
नहीं, बलात्कार के मामलों में पीड़िता की पूर्व यौन गतिविधि को अदालत में उसकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace)
1. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा और न्यायपालिका की भूमिका
- यदि किसी महिला को कार्यस्थल पर अनुचित यौन टिप्पणी, शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाने की मांग, अश्लील सामग्री दिखाने आदि का सामना करना पड़ता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- उदाहरण: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997), मधुरिमा बनाम भारत सरकार।
2. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1997 SC 3011
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैं:
- प्रत्येक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी।
- शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।
- दोषियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
1. इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य और कारण
- महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा से बचाने के लिए।
- घरेलू हिंसा को केवल पत्नी तक सीमित न रखकर, बहन, मां और अन्य महिला रिश्तेदारों को भी सुरक्षा देना।
2. अधिनियम में परिभाषित प्रमुख शब्द:
(a) पीड़ित (Aggrieved Person) – कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो।
(b) घरेलू संबंध (Domestic Relationship) – पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन या ऐसे लोग जो एक साथ रहते हों।
(c) मौद्रिक राहत (Monetary Relief) – पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान।
(d) प्रतिवादी (Respondent) – वह व्यक्ति जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की गई हो।
(e) साझा घर (Shared Household) – वह घर जहां पीड़िता और प्रतिवादी साथ रहते हों या रहते थे।
3. घरेलू हिंसा की परिभाषा (धारा 3)
(i) शारीरिक हिंसा: मारपीट, जलाना, तेजाब डालना आदि।
(ii) मानसिक हिंसा: गाली देना, धमकाना, मानसिक प्रताड़ना देना।
(iii) यौन हिंसा: जबरन शारीरिक संबंध बनाना या उत्पीड़न करना।
(iv) आर्थिक हिंसा: धन रोक लेना, संपत्ति से बेदखल करना आदि।
4. पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य
- पुलिस अधिकारी – तुरंत मामला दर्ज करें और पीड़िता को सुरक्षा दें।
- सेवा प्रदाता – पीड़िता को परामर्श, चिकित्सा और आश्रय गृह की सुविधा दें।
- मजिस्ट्रेट – आरोपी को नोटिस भेजें और आवश्यक राहत दें।
5. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य और कार्य
- नियुक्ति: सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।
- कर्तव्य:
- घरेलू हिंसा की शिकायतें दर्ज करना।
- अदालत में पीड़िता की सहायता करना।
- पीड़िता को पुलिस और अन्य सेवाओं से जोड़ना।
6. सेवा प्रदाता कौन हो सकता है? इसके अधिकार क्या हैं?
सेवा प्रदाता वे पंजीकृत संगठन होते हैं जो घरेलू हिंसा पीड़ितों की सहायता करते हैं।
अधिकार:
- पीड़िता की चिकित्सा और कानूनी सहायता की व्यवस्था करना।
- मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पीड़िता को परामर्श देना।
निष्कर्ष
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून और प्रावधान बनाए गए हैं।
- IPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यौन उत्पीड़न कानून और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- विशाखा दिशानिर्देश, जस्टिस वर्मा रिपोर्ट और 2013 का दंड संशोधन कानून महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत करते हैं।
- कानून का सही क्रियान्वयन ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
7. राहत आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया (Procedure for Obtaining Orders of Reliefs)
- शिकायत दर्ज करना:
- पीड़िता पुलिस, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकती है।
- कोई भी व्यक्ति जो पीड़िता की मदद करना चाहता है, वह भी शिकायत दर्ज कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक जांच:
- मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया मामला देखने के बाद नोटिस जारी कर सकता है।
- यदि आवश्यक हो तो अस्थायी (Interim) राहत आदेश भी दिया जा सकता है।
- उत्तरदाता (Respondent) की सुनवाई:
- प्रतिवादी (आरोपी) को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
- दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अंतिम आदेश जारी करता है।
- राहत आदेश जारी करना:
- संरक्षण आदेश (Protection Order) – प्रतिवादी को पीड़िता से संपर्क करने से रोका जाता है।
- आवास आदेश (Residence Order) – पीड़िता को उसके घर में रहने का अधिकार दिया जाता है।
- मौद्रिक राहत आदेश (Monetary Relief Order) – पीड़िता को आर्थिक सहायता मिलती है।
- अंतरिम आदेश (Interim Order) – तत्काल राहत दी जाती है।
8. कब मजिस्ट्रेट पीड़िता के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी कर सकता है?
मजिस्ट्रेट निम्नलिखित परिस्थितियों में संरक्षण आदेश (Protection Order) जारी कर सकता है:
- यदि पीड़िता को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक या अन्य प्रकार की हिंसा का खतरा है।
- यदि प्रतिवादी पीड़िता का पीछा कर रहा हो, धमकी दे रहा हो या प्रताड़ित कर रहा हो।
- यदि यह आवश्यक हो कि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए।
- यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रतिवादी आदेश का उल्लंघन कर सकता है, तो वह पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश दे सकता है।
संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर:
- 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
9. मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निवास आदेशों का प्रभाव (Effect of Residence Orders)
- पीड़िता को अपने वैवाहिक या पारिवारिक घर में रहने का अधिकार मिलता है, भले ही वह घर प्रतिवादी के नाम पर हो।
- प्रतिवादी (Respondent) को घर छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है यदि वह पीड़िता को प्रताड़ित कर रहा हो।
- प्रतिवादी को घर के किसी विशेष भाग में जाने से रोका जा सकता है।
- प्रतिवादी को घर की संपत्ति नष्ट करने या बेचने से रोका जा सकता है।
- यदि पीड़िता के पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे नया घर देने का आदेश दे सकता है।
10. कब पीड़िता को मौद्रिक राहत दी जा सकती है? यदि प्रतिवादी भुगतान नहीं करता तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा?
- मौद्रिक राहत (Monetary Relief) निम्नलिखित स्थितियों में दी जाती है:
- पीड़िता को आर्थिक रूप से आश्रित होने के कारण भरण-पोषण की जरूरत हो।
- घरेलू हिंसा के कारण चिकित्सा खर्च, संपत्ति की क्षति या अन्य खर्च हुए हों।
- प्रतिवादी जानबूझकर पीड़िता को आर्थिक रूप से असहाय बना रहा हो।
- यदि प्रतिवादी भुगतान नहीं करता है:
- मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के वेतन, बैंक खाता या अन्य संपत्तियों से पैसा काटकर पीड़िता को देने का आदेश दे सकता है।
- यदि प्रतिवादी का कोई नियोक्ता (Employer) है, तो मजिस्ट्रेट उसे आदेश दे सकता है कि वेतन से सीधा भुगतान किया जाए।
- यदि प्रतिवादी के पास कोई कर्जदार (Debtor) है, तो उसे निर्देश दिया जा सकता है कि कर्ज की रकम सीधे पीड़िता को दी जाए।
- आदेश का पालन न करने पर प्रतिवादी को जेल भेजा जा सकता है।
11. अधिनियम में हिरासत आदेश, मुआवजा आदेश और अंतरिम व एकपक्षीय आदेशों का प्रावधान
(a) हिरासत आदेश (Custody Order)
- यदि पीड़िता के बच्चे हैं, तो मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि बच्चों की अस्थायी या स्थायी हिरासत पीड़िता को दी जाए।
- प्रतिवादी को बच्चों से मिलने की सीमित अनुमति दी जा सकती है।
(b) मुआवजा आदेश (Compensation Order)
- यदि पीड़िता को मानसिक या शारीरिक पीड़ा हुई है, तो मजिस्ट्रेट उसे प्रतिवादी से मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता है।
- मुआवजा प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
(c) अंतरिम और एकपक्षीय आदेश (Interim and Ex-Parte Orders)
- यदि स्थिति गंभीर है और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट बिना प्रतिवादी की उपस्थिति के एकपक्षीय आदेश (Ex-Parte Order) जारी कर सकता है।
- अंतरिम आदेश (Interim Order) मामले की अंतिम सुनवाई तक प्रभावी रहता है।
12. (a) संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर क्या दंड है?
- 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
- यदि प्रतिवादी बार-बार उल्लंघन करता है, तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है।
(b) संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य न निभाने पर क्या दंड है?
- यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों।
- संरक्षण अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समय पर जमा करनी होगी, पीड़िता की मदद करनी होगी और कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।
निष्कर्ष:
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कानून महत्वपूर्ण है।
- मजिस्ट्रेट को पीड़िता को राहत देने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार है।
- यदि प्रतिवादी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
- सरकार और संरक्षण अधिकारियों को भी पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।