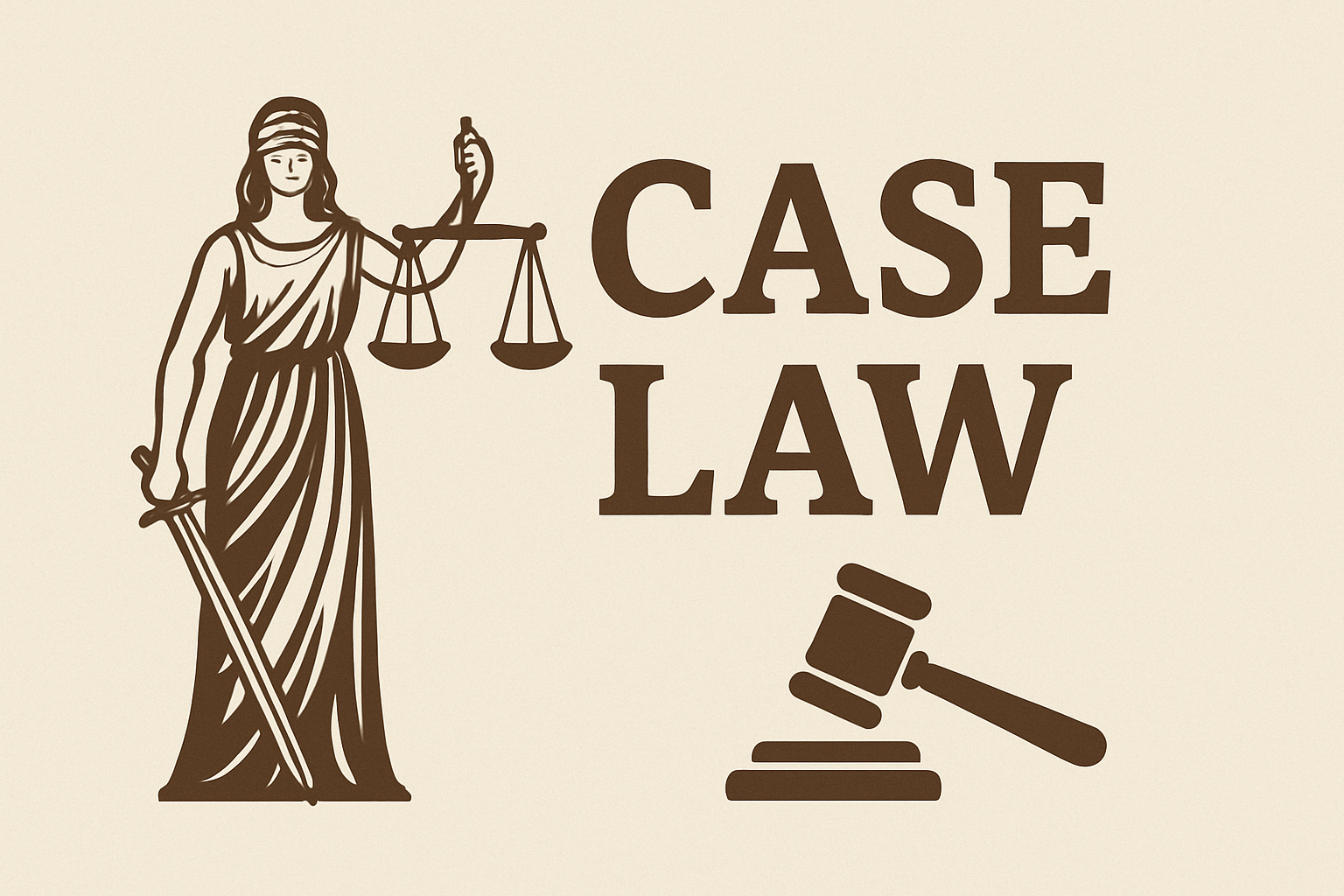Uday v. State of Karnataka (2003, Supreme Court) : सहमति और झूठे वादे पर बलात्कार का न्यायिक दृष्टिकोण
प्रस्तावना
भारतीय दंड संहिता (IPC) में बलात्कार से संबंधित प्रावधान धारा 375 एवं 376 के अंतर्गत आते हैं। समय-समय पर न्यायालयों ने इन धाराओं की व्याख्या करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। Uday v. State of Karnataka (2003) सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला लंबे समय तक अपनी इच्छा और सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है, तो केवल विवाह का झूठा वादा बाद में पूरा न होने पर इसे “झूठे वादे पर बलात्कार” (Rape on false promise of marriage) नहीं माना जा सकता। यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में सहमति (Consent) की अवधारणा को गहराई से स्पष्ट करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अभियुक्त (उदय) ने विवाह का वादा करके पीड़िता से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने विवाह करने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यह “झूठे वादे पर बलात्कार” की श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि विवाह का वादा न किया जाता तो वह संबंध बनाने के लिए सहमत नहीं होती।
ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया, लेकिन मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जहाँ इस मुद्दे पर विस्तृत विचार किया गया कि—
- क्या विवाह का वादा करके सहमति प्राप्त करना “मुक्त और स्वेच्छा से दिया गया सहमति” माना जा सकता है?
- क्या लंबे समय तक बने संबंध वास्तव में ‘झूठे वादे’ का परिणाम थे या परस्पर सहमति से बने थे?
मुख्य विधिक प्रश्न
- क्या विवाह का झूठा वादा ‘सहमति’ को अमान्य कर देता है?
यदि सहमति केवल छल, दबाव या धोखे से प्राप्त की गई है तो उसे वैध नहीं माना जाता। प्रश्न यह था कि विवाह का वादा क्या धोखे की श्रेणी में आएगा। - लंबे समय तक संबंध बनाए जाने की स्थिति में सहमति का स्वरूप क्या माना जाएगा?
यदि महिला बार-बार सहमति देती रही और यह संबंध लंबे समय तक चलता रहा, तो क्या इसे केवल एक धोखे पर आधारित माना जा सकता है? - धारा 375 IPC की परिभाषा में “सहमति” का क्या महत्व है?
क्या विवाह के झूठे वादे से सहमति स्वतः शून्य (invalid) हो जाती है?
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा—
- यदि कोई महिला और पुरुष लंबे समय तक परस्पर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यह केवल विवाह का वादा पूरा न होने की स्थिति में बलात्कार नहीं माना जा सकता।
- अदालत ने माना कि सहमति का अर्थ है “स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से किसी कृत्य को स्वीकार करना।” यदि महिला ने पर्याप्त समय तक सोच-समझकर और बार-बार सहमति दी है, तो बाद में विवाह न होने की स्थिति में यह बलात्कार नहीं कहलाएगा।
- यदि यह सिद्ध हो जाए कि शुरू से ही पुरुष का उद्देश्य केवल धोखा देना था और उसने कभी विवाह करने का इरादा नहीं किया था, तब इसे “झूठे वादे पर बलात्कार” कहा जा सकता है। लेकिन Uday मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला।
निर्णय की न्यायिक विवेचना
- सहमति (Consent) की अवधारणा
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सहमति केवल एक बार नहीं, बल्कि हर बार शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में आवश्यक होती है। यदि महिला ने बार-बार सहमति दी, तो इसे धोखे पर आधारित नहीं माना जा सकता। - धोखे और विश्वासघात में अंतर
यदि कोई पुरुष शुरू से ही विवाह करने का इरादा न रखे और केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए वादा करे, तो यह धोखा होगा। लेकिन यदि उसने ईमानदारी से विवाह का वादा किया और बाद में परिस्थितियाँ बदलने पर विवाह न हो सका, तो यह धोखा नहीं माना जाएगा। - लंबे समय तक संबंध का महत्व
न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई महिला लंबे समय तक सहमति से संबंध रखती है, तो वह केवल झूठे वादे का शिकार नहीं कही जा सकती। इसका मतलब यह है कि उसने स्वेच्छा से संबंधों को स्वीकार किया।
भारतीय न्यायशास्त्र पर प्रभाव
यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में “सहमति” की परिभाषा को और मजबूत करता है। इसके बाद कई अन्य मामलों में अदालतों ने इसी सिद्धांत का पालन किया। उदाहरण के लिए—
- Deepak Gulati v. State of Haryana (2013)
- Dr. Dhruvaram Murlidhar Sonar v. State of Maharashtra (2018)
इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि महिला स्वेच्छा से संबंध बनाती है और बाद में विवाह नहीं हो पाता, तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता।
आलोचना और सीमाएँ
हालाँकि इस निर्णय की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन कुछ आलोचनाएँ भी सामने आईं—
- महिला के अधिकारों की उपेक्षा का आरोप
आलोचकों का कहना था कि इस निर्णय से पुरुषों को यह अवसर मिल सकता है कि वे विवाह का झूठा वादा करके संबंध बनाएँ और बाद में आसानी से बच निकलें। - सामाजिक दबाव और पितृसत्तात्मक व्यवस्था
भारतीय समाज में महिला के लिए विवाह से बाहर संबंध रखना सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यदि महिला ने विवाह की आशा में सहमति दी हो, तो उसकी स्थिति को केवल “स्वेच्छा” कहना उचित नहीं होगा। - झूठे वादे को सिद्ध करने की कठिनाई
अदालत ने यह मानक तय किया कि झूठे वादे पर बलात्कार साबित करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि पुरुष का शुरू से ही धोखा देने का इरादा था। लेकिन इसे व्यवहार में सिद्ध करना अत्यंत कठिन है।
सामाजिक और नैतिक प्रभाव
- इस निर्णय ने यह संदेश दिया कि अदालतें केवल आरोपों के आधार पर पुरुष को दोषी नहीं ठहराएँगी, बल्कि परिस्थितियों और सहमति के वास्तविक स्वरूप की गहराई से जाँच करेंगी।
- इसने यह भी स्पष्ट किया कि महिला को अपने निर्णय की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, यदि वह लंबे समय तक संबंध बनाए रखती है।
- परंतु साथ ही यह चिंता भी बनी रहती है कि कहीं इस सिद्धांत का दुरुपयोग करके महिलाएँ न्याय से वंचित न रह जाएँ।
निष्कर्ष
Uday v. State of Karnataka (2003, SC) भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने स्पष्ट किया कि—
- लंबे समय तक परस्पर सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल विवाह का वादा पूरा न होने की स्थिति में बलात्कार नहीं माना जा सकता।
- सहमति तभी अमान्य होगी जब यह सिद्ध हो जाए कि शुरू से ही पुरुष का इरादा धोखा देने का था।
यह निर्णय सहमति (Consent) और धोखे (Deception) के बीच संतुलन स्थापित करता है। हालांकि इसमें कुछ कमजोरियाँ भी हैं, परंतु यह भारतीय न्यायशास्त्र में बलात्कार और सहमति से जुड़े मामलों का मार्गदर्शक निर्णय है।
1. इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
Uday v. State of Karnataka (2003) में अभियुक्त पर आरोप था कि उसने विवाह का वादा करके पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह करने से इंकार कर दिया। पीड़िता का कहना था कि यह विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार है। निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया, परंतु मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या विवाह का झूठा वादा स्वतः सहमति को अमान्य कर देता है और क्या लंबे समय तक सहमति से बने संबंध बलात्कार की श्रेणी में आ सकते हैं।
2. इस मामले में मुख्य विधिक प्रश्न क्या थे?
मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या विवाह का वादा करके प्राप्त सहमति को धोखे पर आधारित माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह था कि यदि महिला लंबे समय तक सहमति से संबंध बनाए रखती है, तो क्या बाद में विवाह न होने पर इसे बलात्कार माना जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि धारा 375 IPC में परिभाषित “सहमति” की व्याख्या किस प्रकार होगी और कब यह वैध मानी जाएगी।
3. सुप्रीम कोर्ट ने सहमति (Consent) को कैसे परिभाषित किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति का अर्थ है स्वतंत्र और स्वेच्छा से किसी कृत्य को स्वीकार करना। यदि महिला ने लंबे समय तक सोच-समझकर और बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति दी है, तो इसे केवल विवाह के वादे पर आधारित सहमति नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सहमति तभी अमान्य होगी जब यह साबित हो जाए कि शुरू से ही पुरुष का उद्देश्य धोखा देना था।
4. लंबे समय तक बने संबंधों को अदालत ने कैसे देखा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला लंबे समय तक परस्पर सहमति से संबंध रखती है, तो वह केवल झूठे वादे की शिकार नहीं कही जा सकती। यह उसकी स्वतंत्र पसंद और निर्णय को दर्शाता है। विवाह न होने की स्थिति में यह स्वतः बलात्कार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि महिला ने अपने विवेक और स्वेच्छा से इन संबंधों को स्वीकार किया था।
5. अदालत ने धोखे और विश्वासघात में क्या अंतर किया?
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पुरुष शुरू से ही विवाह करने का इरादा न रखे और केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए झूठा वादा करे, तो यह धोखे का मामला होगा और इसे बलात्कार माना जा सकता है। लेकिन यदि पुरुष वास्तव में विवाह करना चाहता था परंतु बाद में परिस्थितियों के कारण विवाह नहीं हो पाया, तो इसे धोखा नहीं कहा जा सकता।
6. इस मामले का भारतीय न्यायशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा?
यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में सहमति (Consent) की व्याख्या का महत्वपूर्ण मानक बना। इसके बाद Deepak Gulati v. State of Haryana (2013) और Dr. Dhruvaram Sonar v. State of Maharashtra (2018) जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत अपनाया। अदालतों ने बार-बार कहा कि केवल विवाह न होने पर इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता, जब तक कि प्रारंभ से धोखे का इरादा न हो।
7. इस निर्णय की आलोचना क्यों हुई?
कुछ विद्वानों ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करता है, क्योंकि पुरुष विवाह का झूठा वादा करके आसानी से संबंध बना सकते हैं और बाद में बच सकते हैं। साथ ही, भारतीय सामाजिक संदर्भ में महिला की स्थिति को देखते हुए यह कहना कि उसने स्वतंत्र सहमति दी, हमेशा व्यावहारिक नहीं है। आलोचना यह भी थी कि शुरू से धोखे का इरादा साबित करना अत्यंत कठिन होता है।
8. सामाजिक दृष्टि से इस निर्णय का क्या महत्व है?
इस निर्णय ने यह संदेश दिया कि अदालत केवल आरोपों के आधार पर पुरुष को दोषी नहीं ठहराएगी, बल्कि परिस्थितियों और सहमति के वास्तविक स्वरूप की गहराई से जाँच करेगी। यह महिला की स्वतंत्रता और पुरुष की जिम्मेदारी दोनों को संतुलित करता है। हालाँकि, यह भी चिंता बनी रही कि कहीं इस सिद्धांत का दुरुपयोग न हो और महिलाएँ न्याय से वंचित न रह जाएँ।
9. बलात्कार के मामलों में सहमति की क्या भूमिका है?
धारा 375 IPC के अनुसार, यदि शारीरिक संबंध महिला की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए जाते हैं, तभी यह बलात्कार होगा। Uday केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति केवल एक बार नहीं बल्कि हर बार आवश्यक है। यदि महिला ने बार-बार सहमति दी, तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। सहमति तभी अवैध होगी जब यह धोखे या दबाव से ली गई हो।
10. निष्कर्ष रूप में इस केस की क्या अहमियत है?
Uday v. State of Karnataka (2003) ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि लंबे समय तक परस्पर सहमति से बने संबंध विवाह न होने पर बलात्कार नहीं कहे जा सकते। सहमति को अमान्य तभी माना जाएगा जब यह सिद्ध हो कि शुरू से ही पुरुष का उद्देश्य धोखा देना था। यह निर्णय सहमति और धोखे के बीच की रेखा को स्पष्ट करता है और भारतीय दंड कानून में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।