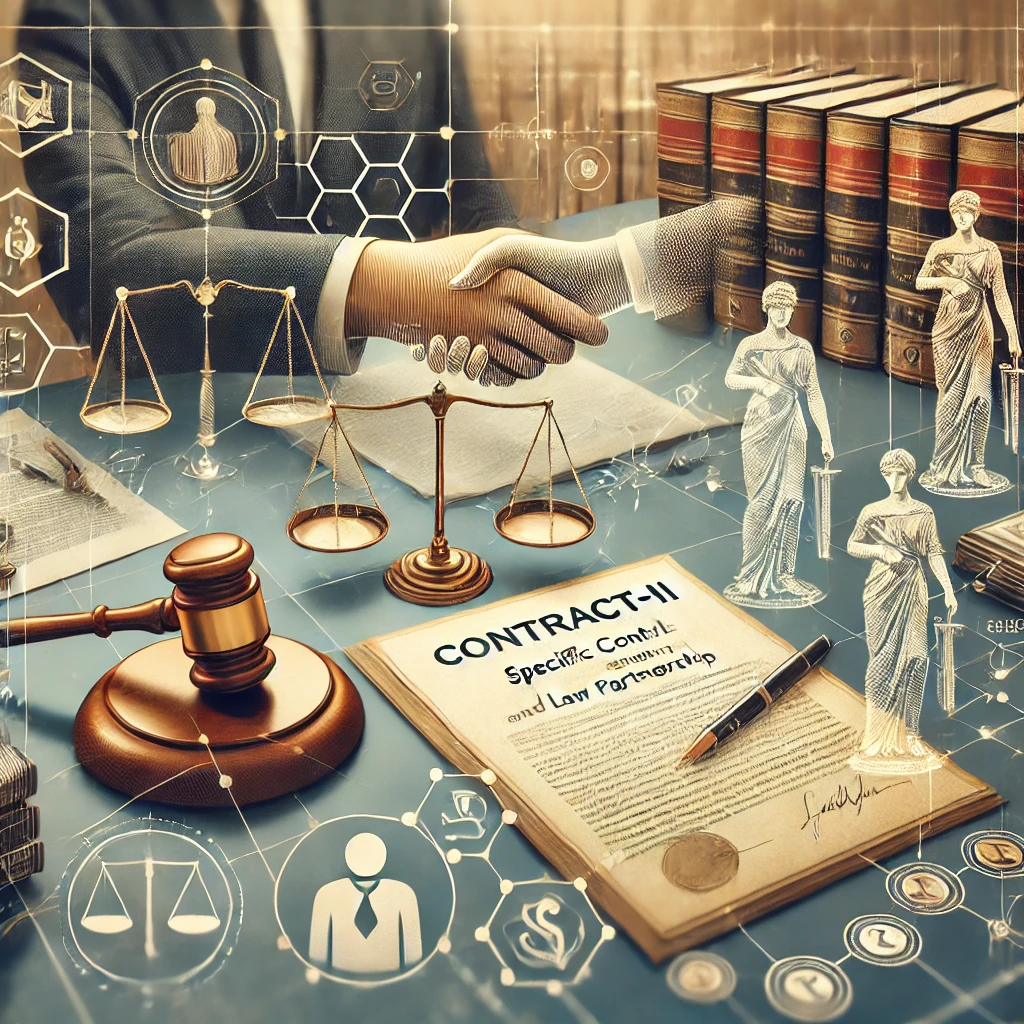प्रश्न 1. क्षतिपूर्ति की संविदा से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by Contract of Indemnity?
उत्तर – क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, “क्षतिपूर्ति की संविदा” कहलाती है। इस प्रकार इस संविदा में, पक्षकारों के बीच एक सीधा सम्बन्ध स्थापित होता है। एक पक्षकार जो बचाने या क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा करता है, उसे क्षतिपूर्तिदाता (Indemnifier) तथा दूसरा पक्षकार जिसको क्षतिपूर्ति की जाती है, को क्षतिपूर्तिधारी (Indemnity holder) कहते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षतिपूर्तिधारी को अपने आचरण से, या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचायेगा। जैसे-‘राम’, ‘श्याम’ को उस कार्यवाही से हुई हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है जो कार्यवाही ‘वन्दना’, ‘श्याम’ के विरुद्ध 2,000 रुपये के सम्बन्ध में चलायेगा। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है।
प्रश्न 2. क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों को इंगित कीजिए।
Point out the rights of a Indemnity holder.
उत्तर– क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार – भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 के अनुसार, क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रतिज्ञाग्रहीता अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता हुआ प्रतिज्ञाकर्ता से निम्न क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है
(1) क्षतिपूर्तिधारी (प्रतिज्ञाग्रहीता) यदि किसी बात से सम्बन्धित चलाये गये वाद में यदि कोई नुकसानी या क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया गया है जिसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की संविदा की गई है तो वह क्षतिपूर्तिदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) से नुकसानी या प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई राशि को प्राप्त कर सकता है।
(2) प्रतिज्ञाग्रहीता (क्षतिपूर्तिधारी) किसी वाद की लागत या खर्च भी प्रतिज्ञादाता (क्षतिपूर्तिदाता) से प्राप्त कर सकता है, यदि क्षतिपूर्तिदाता (प्रतिज्ञादाता) ने क्षतिपूर्तिधारी (प्रतिज्ञाग्रहीता) को वाद चलाने या बचाव करने हेतु अधिकृत किया हो। यदि वाद के संचालन या बचाव करने में प्रतिज्ञादाता (क्षतिपूर्तिदाता) के आदेशों का उल्लंघन न किया हो तथा क्षतिपूर्तिधारी ने एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की भाँति कार्य किया है।
(3) प्रतिज्ञाग्रहीता (क्षतिपूर्तिधारी) वह धनराशि प्रतिज्ञाकर्ता (क्षतिपूर्तिदाता) से प्राप्त कर सकता है जो उसने मुकदमे के समझौते के अन्तर्गत भुगतान किया है। यदि यह समझौता प्रतिज्ञादाता (क्षतिपूर्तिदाता) के आदेशों के उल्लंघन में नहीं किया प्रकार का समझौता करता यदि वह समझौता करने हेतु अधिकृत किया गय होता।
प्रश्न 3 प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Contract Guarantee?
उत्तर- प्रत्याभूति की संविदा – भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 के अन्ता प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित किया गया है। प्रत्याभूति की संविदा से तात्पर्य एक ऐसी संविदा से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (चूक) व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा (सूचन) के पालन या उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है ‘प्रतिभू’ कहलाता है, वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है. “मूलऋणी” कहलाता है और यह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, ‘लेनदार’ कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी अर्थात् यह एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायित्व लेता है।
‘क’, ‘ख’ से 50,000 रुपया उधार लेता है तथा उसे तीन वर्ष के भीतर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। ‘ग’ ‘ख’ को यह वचन देता है कि यदि ‘क’ तीन वर्ष के अन्दर 50,000 रुपया वापस नहीं करता है तो वह 50,000 रुपया वापस करेगा। यह ‘ग’ तथा ‘ख’ के मध्य हुई संविदा प्रत्याभूति की संविदा हुई।
प्रश्न 4. क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रत्याभूति की संविदा में क्या अन्तर है?
What is the difference between Contract of Indemnity and Contract of Guarantee?
उत्तर- क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर-प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं जबकि क्षतिपूर्ति में दो ही पक्षकार होते हैं। प्रत्याभूति को संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है। प्रत्याभूति मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है जबकि क्षतिपूर्ति की संचिदा तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं होती है। प्रतिभू मूल ऋणी का ऋण चुकाकर मूल ऋणी पर रकम वसूली का दावा कर सकता है जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा के अन्तर्गत क्षतिपूरक किसी से भी रकम वसूल नहीं कर सकता है।
प्रश्न 5 प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन किस तरह होता है?
How does the discharge of surety’s liability?
उत्तर- प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन – कोई प्रतिभू अपने दायित्व से निम्नलिखित परिस्थितियों में मुक्त हो जाता है- (1) प्रत्याभूति का खण्डन करने (प्रतिसंहरण • Revocation) के द्वारा (2) प्रतिभू की मृत्यु होने पर (3) मूल ऋणी तथा लेनदार के मध्य संविदा की पूर्ति में परिवर्तन करने पर (4) मूल ऋणी (Principal Debtor) के उन्मोचन पर (5) लेनदार द्वारा मूल ऋणी के समझौता करने या उसे समय देने या उसके द्वारा मूल ऋणों पर वाद न करने के करार करने पर तथा (6) लेनदार द्वारा ऐसा कार्य या चूक करने पर जिससे प्रतिभू को प्राप्त अधिकार समाप्त हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
प्रश्न 6 शर्त और प्रत्याभूति को परिभाषित कीजिए। शर्त और प्रत्याभूति में अन्तर बतलाइए।
Define conditions and warranty. Distinguish between to condition and warranty.
उत्तर- शर्त एवं प्रत्याभूति की परिभाषा – संविदा के निर्माण में शर्तों का अपना महत्व है। परन्तु प्रत्येक शर्त का महत्व समान नहीं होता। इनमें से कुछ शर्तें ऐसी होती हैं। जिनका पालन कठोरतापूर्वक अनिवार्य है तथा इनका पालन न होने से संविदा सारवान् रूप से प्रभावित होती है। इनका पालन होने से संविदा का पालन नहीं माना जाता। इन्हें शर्त का नाम दिया गया है। इनके पालन न होने के आधार पर संविदा के एक पक्षकार को यह अधिकार होता है कि वह पूरी संविदा को विखण्डित (repudiate) कर दे। परन्तु संविदा पालन की ऐसी शर्त जिसका संविदा पालन में उतना महत्व नहीं होता, उसे वारण्ट या आश्वासन या प्रत्याभूति कहा जाता है। इसके पालन न होने से संविदा का विखण्डन नहीं किया जा सकता परन्तु इसके पालन न होने से व्यथित पक्षकार को सिर्फ क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त होता है।
शर्त तथा वारण्टी में अन्तर
( Difference between Condition & Warranty )
शर्त (Condition)
(i) शर्त माल विक्रय की एक महत्वपूर्ण तथा सारवान् अनुबन्ध होती है।
(ii) शर्त का उल्लंघन व्यथित पक्षकार को माल वापस कर मूल्य वापस पाने का अधिकार देती है ।
(iii) शर्त के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह संविदा को निरस्त (repudiate) कर सके।
वारण्टी (आश्वासन या प्रत्याभूति) (Warranty)
(i) वारण्टी माल विक्रय की संविदा का साम्पार्रिवक (colleteral) अनुबन्ध होता है।
(ii) वारण्टी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार सिर्फ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
(iii) वारण्टी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार विक्रय की संविदा का विखण्डन नहीं कर सकता वह सिर्फ क्षतिपूर्ति की माँग कर सकता है।
प्रश्न 7. चलत प्रतिभूति क्या है?
What is Continuing Guarantee?
उत्तर- चलत प्रतिभूति– संविदा अधिनियम की धारा 129 में चलत प्रतिभूति (Continuing Guarantee) की परिभाषा दी गयी है। इसके अनुसार जब प्रत्याभूति का विस्तार एक संव्यवहार तक सीमित न होकर कई संव्यवहारों के कई भागों (आवली) तक विस्तृत रहता है तो उसे चलत प्रत्याभूति कहते हैं।
जैसे-‘राम’ एक चाय के व्यापारी ‘शिवांश’ को, उसे चाय के लिए, जिसका वह ‘हर्ष’ को समय-समय पर प्रदाय करे, 100 पौण्ड तक की रकम का संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। ‘हर्ष’ को ‘शिवांश’ उपर्युक्त 100 पौण्ड से अधिक मूल्य की चाय का प्रदाय करता है और “हर्ष” उसके लिए ‘शिवांश को संदाय कर देता है। तत्पश्चात् ‘हर्ष’ को शिवांश 200 पौण्ड मूल्य की चाय का प्रदाय करता है। ‘हर्ष’ रकम संदाय करने में असफल रहता है। राम द्वारा दो गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति थी और तदनुसार वह ‘शिवांश’ को प्रति 100 पौण्ड तक ही दायी है।
प्रश्न 8. चलत प्रत्याभूति एवं विशिष्ट प्रत्याभूति में अन्तर कीजिए।
Difference between a continuing guarantee and a specific guarantee.
उत्तर- चलत प्रत्याभूति एवं विशिष्ट प्रत्याभूति में अन्तर- जब प्रत्याभूति का विस्तार एक संव्यवहार तक सीमित न होकर कई संव्यवहार के कई भागों (आवली) पर विस्तारित रहता है तो उसे चलत प्रत्याभूति कहते हैं। जबकि जो प्रत्याभूति केवल एक संव्यवहार के लिए दी गई हो, वह उस संव्यवहार के पूरे होते ही समाप्त हो जाती है, उसे विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। जैसे-‘हर्ष’, ‘शिवांश’ को यह वचन देता है कि यदि वह (शिवांश) ‘ऋषभ’ को 10,000 रुपये ऋण के रूप में देगा तो यदि ‘ऋषभ द्वारा ऋण वापस करने में चूक की जाती है तो उक्त स्थिति में ऋण की राशि वह (हर्ष) ‘शिवांश’ को वापस कर देगा। यह एक विशिष्ट प्रत्याभूति है जो केवल एक संव्यवहार के रूप में दी गई है। यह प्रत्याभूति जिस संव्यवहार के विषय में दी जाती है, उसके पूर्ण होते ही समाप्त हो जाती है।
प्रश्न 9. चलत प्रत्याभूति के प्रतिसंहरण की व्याख्या कीजिए। Describe the revocation of continuing guarantee.
उत्तर- चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण (धारा 130) – संविदा अधिनियम को धारा 130 चलत प्रत्याभूति के प्रतिसंहरण के विषय में बतलाती है। इस धारा के अनुसार, “चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी समय भी प्रतिभू कर सकेगा।”
अतः चलत प्रत्याभूति के प्रतिसंहरण का प्रथम तरीका यह है कि प्रतिभू भविष्य के संव्यवहारों के लिए प्रतिसंहरण की सूचना देकर अपने द्वारा दी गई प्रत्याभूति को वापस ले सकता है। भविष्य में कोई ऋण या वस्तुओं को देने के लिए दी गई प्रत्याभूति तभी बाध्यकारी होगी जबकि उस व्यक्ति ने जिसको प्रत्याभूति दी गई है, उस पर कार्य किया हो। परन्तु उस पर कार्य किये जाने के पूर्व प्रत्याभूति वापस ली जा सकती है। कार्य किये जाने के बाद भी शेष संव्यवहारों के लिए प्रत्याभूति वापस ली जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक संव्यवहार स्वतन्त्र होता है।
प्रश्न 10. निक्षेप या उपनिधान से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Bailment?
उत्तर- निक्षेप या उपनिधान – भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 निक्षेप या उपनिधान की परिभाषा देती है। जब एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए अपनी किसी वस्तु को इस संविदा (शर्त) के साथ देता है कि दूसरा व्यक्ति उस प्रयोजन को पूर्ण होने के पश्चात् वस्तु (माल) का परिदान करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा निर्देशित किसी दूसरे व्यक्ति को वापस दे देगा तो ऐसी संविदा को उपनिधान की संविदा कहते हैं।
कपड़े दर्जी को सीने के लिए देना, कपड़े ड्राइक्लिनिंग के लिए ड्राइक्लीनर को देना, साइकिल या घड़ी मरम्मत हेतु देना, आभूषण निर्माण हेतु सोना या चाँदी देना उपनिधान संविदा के कुछ उदाहरण हैं।
जो व्यक्ति माल या वस्तु को किसी उद्देश्य के लिए परिदत्त करता है उसे उपनिधाता या निक्षेपक (Bailor) कहते हैं तथा जिस व्यक्ति को वस्तु या माल का परिदान किया जाता है वह उपनिहिती या निक्षेपग्रहीता कहलाता है।
प्रश्न 11. उपनिधान के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। Explain the elements of Bailment briefly.
उत्तर- एक वैध उपनिधान के लिए आवश्यक तत्व हैं :
( 1 ) वस्तु या माल के कब्जे का एक व्यक्ति (वस्तु के स्वामी) से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण– उपनिधान का सबसे आवश्यक तत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु के कब्जे का अन्तरण है। इस प्रकार उपनिधान सिर्फ चल (जंगम) सम्पत्ति का हो सकता है। | उपनिधान में वस्तु का स्वामित्व वस्तु के स्वामी (उपनिधाता) के पास बना रहता है। कब्जे का अन्तरण (परिदान) वास्तविक (Actual) तथा विवक्षित (Constructive) दोनों प्रकार से हो सकता है।
(2) वस्तु का परिदान इस शर्त के साथ होना आवश्यक है कि वस्तु उस प्रयोजन के पूरा होने के पश्चात् उपनिधाता (स्वामी) या उपनिधाता द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को लौटा दी जायेगी – यही आवश्यक तत्व उपनिधान की संविदा को विक्रय तथा दान की संविदा से पृथक् करता है। विक्रय तथा दान को संविदा में वस्तु का स्थायी परिदान (अन्तरण) होता है परन्तु उपनिधान में वस्तु का अन्तरण या परिदान अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस शर्त पर होता है कि प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर वस्तु (स्वामी) उपनिधाता को लौटा दी जाय।
प्रश्न 12. उपनिधाता एवं उपनिहिती के क्या कर्तव्य हैं?
What are duties of Bailor and Bailee?
उत्तर– वस्तु या माल में निहित त्रुटियों को प्रकट करना आवश्यक खर्चों का भुगतान करना, उपनिधान के समय से पूर्व वस्तु वापस माँगने पर क्षतिपूर्ति करना तथा उपनिधान करने का अधिकार न होने के कारण होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करना उपनिधाता के प्रमुख कर्त्तव्य हैं।
संविदा अधिनियम की धारा 151 के अनुसार उपनिहिती का यह कर्त्तव्य होता है कि उपनिधान की वस्तु के प्रति उचित सावधानी बरते तथा उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक प्रयोग न करे और उपनिधाता की वस्तु का अपनी वस्तु के साथ मिश्रण न करे, उपनिधान की वस्तु को वापस कर दे, उपनिधान के अधिकार की अवहेलना न करे, उपनिधान को वस्तु में उपनिधान की अवधि में हुई क्षति या लाभ को लौटा दे।
प्रश्न 13. उपनिधाता के अधिकारों की विवेचना कीजिये।
Discuss the rights of the Bailor.
उत्तर– उपनिधाता के अधिकार- उपनिधाता के निम्न अधिकार हैं –
(1) संविदा अधिनियम की धारा 151 तथा 152 के अनुसार यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई वस्तु के प्रति उतनी सतर्कता या सावधानी नहीं बरतता जितनी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वैसी वस्तु के प्रति बरतता तो यदि उपनिहिती की असावधानी के कारण उपनिहिती द्वारा वस्तु को कोई क्षति होती है तो उस क्षति को उपनिधाता प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
(2) यदि उपनिहिती (Bailee) उपनिधान की वस्तु को ऐसे प्रयोग करता है जो उपनिधान की शर्त के अनुसार असंगत (inconsistant) है तो उपनिधान उपनिधाता समाप्त करवा सकता है।
(3) संविदा अधिनियम की धारा 154 के अनुसार, यदि उपनिहिती उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक (Unnatural) प्रयोग करता है तथा इस अप्राकृतिक प्रयोग के कारण वस्तु (माल) को कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार उपनिधाता को होगा।
(4) संविदा अधिनियम की धारा 157 के अनुसार, यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई उपनिधाता की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रित करता है तो (अ) यदि इस मिश्रण को पृथक् किया जाना सम्भव है तो उसे पृथक् करने में हुए खर्च को उपनिधाता वसूल कर सकता है; (ब) यदि उस मिश्रण का पृथक् किया जाना सम्भव नहीं है तो उपनिधाता उपनिहिती से इस मिश्रण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
(5) संविदा अधिनियम की धारा 161 के अनुसार यदि उपनिधान किसी निश्चित समय के लिए है तथा उपनिधाता द्वारा निश्चित समय के पश्चात् वस्तु वापस करने की माँग की जाती है तथा उपनिहिती वस्तु को माँगने पर वापस करने में असफल रहता है या यदि उपनिधान निःशुल्क है तथा उपनिधाता द्वारा किसी समय वस्तु वापस माँगने पर उपनिधान की वस्तु उपनिहिती वापस करने में असफल रहता है तो उपनिहिती द्वारा वस्तु वापस न कर पाने के कारण उपनिधाता को जो क्षति होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार उपनिधाता को होगा।
(6) संविदा अधिनियम की धारा 163 के अनुसार, यदि उपनिधान की वस्तु वृद्धि या उससे कोई लाभ उपनिहिती को हुआ है तो उपनिधाता उसे प्राप्त करने का अधिकार रखता है यदि उसके प्रतिकूल उनके मध्य कोई संविदा नहीं हुई है।
प्रश्न 14. धारणाधिकार कितने प्रकार का होता है?
What are different kinds of Right of lien?
उत्तर– धारणाधिकार दो प्रकार का होता है- (1) साधारण धारणाधिकार (General Right of Lien); और (ii) विशिष्ट धारणाधिकार (Particular Right of Lien)
साधारण धारणाधिकार (General Right of Lien)– साधारण धारणाधिकार का उल्लेख अधिनियम की धारा 171 में किया गया है। इसके अनुसार साधारण धारणाधिकार के अन्तर्गत उपनिहिती को उपनिधाता की कोई भी वस्तु जो उसके पास है, रोकने का अधिकार है। भले ही किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में हुआ हो। धारा 171 के अनुसार साधारण धारणाधिकार केवल बँकर, आढ़तिया घाटवाल, उच्च न्यायालय के एडवोकेट तथा बीमा के दलाल को ही प्राप्त है।
विशिष्ट धारणाधिकार (Particular Right of Licn) – विशिष्ट धारणाधिकार के अन्तर्गत उपनिहिती को सिर्फ उस विशिष्ट वस्तु को रोकने का अधिकार है जिस पर कार्य हुआ हो धारा 170 के अनुसार यदि उपनिहिती ने उपनिहित वस्तु के सम्बन्ध में उपविधान के प्रयोजन के अनुसार कोई सेवा की है जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग करना था तो उसे उस विशिष्ट वस्तु को तब तक रोकने का अधिकार है जब तक उस सेवा या परिश्रम का मूल्य न मिल जाय परन्तु यदि उसके प्रतिकृत कोई संविदा है तो वह संविदा ही प्रभावी होगी।
प्रश्न 15 गिरवी की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्व बतलाइये।
Define Pledge and explain its Essential Elements.
उत्तर- गिरवी (Pledge) – संविदा अधिनियम की धारा 172 में गिरवी (Pledge) की परिभाषा दी गयी है। इस धारा के अनुसार-किसी ऋण को देने के लिए या किसी अन्य वचन के पालन के लिए प्रतिभूति (guarantee) के रूप में माल (वस्तु) के उपनिधान को गिरवी कहते हैं।
एक वैध गिरवी के आवश्यक तत्व – एक वैध गिरवी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व (Essentials) होने चाहिए –
(1) बस्तु (माल) का उपनिधान किया जाना चाहिए तथा
(2) वस्तु का उपनिधान ऋण के भुगतान या किसी बचन के पालन के प्रतिभूति के लिए किया जाना चाहिए।
प्रश्न 16. उपनिधान एवं गिरवी में अन्तर कीजिए।
Differentiate between Bailment and Pledge.
उत्तर– उपनिधान एवं गिरवी में अन्तर- उपनिधान एवं गिरवी में मुख्य अन्तर निम्न प्रकार से है- (1) उपनिधान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जायेगा तब वह लौटा दिया जायेगा या उस परिदान करने वाले के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित किया जायेगा जबकि,
गिरवी में किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है।
(2) उपनिधान में जब उपनिधाता, उपनिहिती द्वारा किये गये विधिक व्ययों व खर्चों का भुगतान नहीं करता तो उपनिहिती माल को रोक सकता है जिसे उपनिहिती का धारणाधिकार कहते हैं।
गिरवी में यदि पणयमकार उस ऋण का संदाय करने में या निश्चित समय पर उस बचन का पालन करने में जिस हेतु माल गिरवी रखा गया है, चूक करता है तो पणयमकार को युक्तियुक्त सूचना देकर गिरवी माल का विक्रय कर सकता है।
प्रश्न 17. गुडविल क्या है? What is goodwill?
उत्तर- गुडविल (Goodwill)– किसी भागीदारी फर्म का ख्याति (Goodwill) उसकी सम्पत्ति ही नहीं अपितु अति महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। एक भागीदारी फर्म अपने व्यापारिक जीवन में अपने भागीदारों के माध्यम से भागीदारों की ईमानदारी, उनके व्यापारिक कौशल तथा कार्य करने के ढंग के आधार पर व्यापारिक जगत में जो प्रतिष्ठा अर्जित करती है, उसे फर्म की ख्याति या गुडविल कहते हैं। फर्म की ख्याति या प्रतिष्ठा फर्म को व्यापार जगत में उसे स्थापित करने में तथा उसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित करती है। किसी शहर में किसी फर्म के नाम से ग्राहक उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। यह उस फर्म की गुडविल का ही प्रतिफल होता है। गोरखपुर में एक जमाने में चौधरी स्वीट हाउस का मिष्ठान्न विक्रय तथा जल-पान के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान था। इसकी मिठाई दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी प्रकार वाराणसी में कन्हैया स्वर्ण अलंकार मंदिर आभूषण विक्रय के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिष्ठा रखती है। यहाँ दूर दराज से लोग आभूषण क्रय करने आते हैं। यहाँ ख्याति या गुडविल निरन्तर सदाचरण तथा उनके द्वारा विक्रय की जाने वाले वस्तुओं की निरन्तर गुणवत्ता के आधार पर कई वर्षों में अर्जित होती है। ऊन के क्षेत्र में लाल इमली तथा कपड़ों के क्षेत्र में सेन्चुरी मिल, अरविन्द मिल की ख्याति भी एक विशिष्ट स्थान रखती है। टाटा तथा बाटा के नाम भी गुडविल या ख्याति के उदाहरण हैं। गुडविल का अस्तित्व ग्राहकों के आंकलन में निहित होता है। गुडविल का संरक्षण ग्राहकों का संरक्षण है।
प्रश्न 18. अभिकर्ता कौन है? विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं को परिभाषित कीजिए।
Who is an Agent? Define various kinds of Agents.
उत्तर- अभिकर्ता (Agent) – संविदा अधिनियम की धारा 182 अभिकर्ता (Agent) तथा स्वामी (Principal) की परिभाषा देती है। इस परिभाषा के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से संव्यवहारों (Transactions) में किसी अन्य (जिसके द्वारा नियोजित है-स्वामी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित (Employed) है।
संक्षेप में अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक की ओर से कार्य करने हेतु या मालिक का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोजित होता है। अभिकर्त्ता अपने स्वामी की ओर से कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से बाध्य कर सकता है परन्तु मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से अभिकर्त्ता तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक इस विषय में उसकी स्वामी के साथ पृथक् संविदा न हो।
अभिकर्त्ता होने के लिए संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक नहीं है। अतः एक अवयस्क अभिकर्ता हो सकता है परन्तु एक अवयस्क व्यक्ति स्वामी (मालिक) नहीं हो सकता।
अभिकर्त्ता के प्रकार (Kinds of Agent)- सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अभिकर्त्ता निम्न प्रकार के हो सकते हैं –
(1) सामान्य अभिकर्त्ता– सामान्य अभिकर्ता वह है जो एक निश्चित सीमा या क्षेत्र के अन्तर्गत स्वामी की ओर से कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है।
(2) विशिष्ट अभिकर्त्ता – विशिष्ट अभिकर्ता वह है जो स्वामी द्वारा किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए नियोजित होता है जिसका उल्लेख उसके नियोजन के साथ किया गया हो ऐसे अभिकर्ता द्वारा किए गए उस विशिष्ट कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया था।
(3) सार्वभौमिक अभिकर्त्ता– वह है जो अपने स्वामी की ओर से वे सभी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है जो वैध तथा विधिसम्मत हो सार्वभौमिक अभिकर्ता (Universal agent) का अधिकार असीमित होता है।
प्रश्न 19. एक अभिकर्ता के कर्तव्य तथा अधिकार बताइए। Explain the rights and duties of an agent.
उत्तर– अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अपने स्वामी के लिए अपने स्वामी की ओर से कार्य करता है। इस प्रकार अभिकर्ता स्वामी के लाभ के लिए स्वामी के हित में कार्य करे, ऐसी अपेक्षा उससे रखी जाती है।
अभिकर्त्ता के कर्त्तव्य- सामान्यतः एक अभिकर्ता के उसके स्वामी के प्रति कर्तव्य का निर्धारण अधिकरण के लिए उनके मध्य संविदा की शर्तों के आधार पर निर्भर करता है। परन्तु संविदा को शर्तों के अधीन रहते हुए एक अभिकर्ता का अपने स्वामी के प्रति निम्न कर्तव्य होते हैं –
(1) स्वामी के आदेश तथा स्वामी के व्यापार की रूढ़ियों के अनुसार कार्य करने का कर्त्तव्य (धारा 211);
(2) स्वामी द्वारा सौंपे गये कार्य को करने का कर्त्तव्य;
(3) उचित तत्परता तथा कौशल्य प्रयोग करने का कर्तव्य;
(4) स्वामी की सम्मति के बिना अपने हित में कार्य न करने का कर्तव्य;
(5) गुप्त लाभ प्राप्त न करने का कर्तव्य;
(6) स्वामी के निमित्त प्राप्त राशियों को वापस करने का कर्त्तव्य तथा
(7) अपना कार्य किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपने का कर्त्तव्य;
अभिकर्त्ता के अधिकार – एक अभिकर्ता के निम्न अधिकार हैं-
(1) पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार [यदि अभिकर्त्ता कदाचार (Misconduct) का दोषी है तो वह पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता (धारा 220)];
(2) राशि को रोकने का अधिकार (धारा 217):
(3) धारणाधिकार (धारा 221);
(4) क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार (धारा 222 तथा 223) ; तथा
(5) प्रतिकर प्राप्त करने का अभिकर्त्ता का अधिकार (धारा 225)।
प्रश्न 20. अभिकर्ता के अवैध कार्यों के लिए दायित्व का उल्लेख करें।
Explain the liability for illegal works of Agent.
उत्तर- अभिकर्ता के अवैध कार्यों के लिए दायित्व (धारा 238) अपने कारबार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्त्ताओं द्वारा किये गये दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किये गये करारों पर वही प्रभाव रखते हैं मानों ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किये गये हों। किन्तु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में, जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते, किये गये दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि इस धारा के दृष्टान्त (क) एवं (ख) में दिया गया है –
(क) क. जो माल के विक्रय के लिये ख का अभिकर्त्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा जिसे करने के लिए वह ‘ख’ द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहाँ तक कि ख और ग के बीच का सम्बन्ध है, संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है।
(ख) ख के पोत का कप्तान के वहनपत्रों पर उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किये बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहाँ तक ख और अपदेशी पारेषक का सम्बन्ध है, वे वहनपत्र शून्य हैं।
अर्थात् अभिकर्त्ता द्वारा किये गये दुर्व्यपदेशन व कपट के लिए मालिक का दायित्व केवल निम्न विषय में होगा –
(क) जो विषय मालिक के प्राधिकार के अन्तर्गत आते हों,
(ख) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में हों, तथा
(ग) मालिक के लिए किए गये हों,
फुलर बनाम विल्सन (1842) 3 C.B. 58 के बाद में मकान मालिक ने अपने मकान के विक्रय हेतु एक अभिकर्त्ता नियुक्त किया। अभिकर्त्ता ने क्रेता को सूचित किया कि मकान कर मुक्त है, यद्यपि उसे ऐसी जानकारी भी थी। मालिक यह जानता था कि मकान कर मुक्त है। क्रेता द्वारा मकान क्रय किए जाने पर कर लगा दिया गया। अत: मालिक दिए गये कर के लिए दायी होगा। न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि इस संव्यवहार में क्रेता को वास्तव में धोखा दिया गया था, तो कानून उसे संरक्षण प्रदान करेगा। संव्यवहार के लिए मालिक व अभिकर्ता एक ही व्यक्ति माने जाते हैं।
प्रश्न 21. स्थानापन्न अभिकर्ता की परिभाषा दीजिए।
Define Substituted Agent.
उत्तर- स्थानापन्न अभिकर्त्ता – प्रतिस्थापित या स्थानापन्न अभिकर्त्ता वह व्यक्ति होता है जो मालिक की प्रार्थना पर स्पष्ट व विवक्षित प्राधिकार से अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार वह स्वामी का अभिकर्ता होता है। यद्यपि इसकी नियुक्ति अभिकर्त्ता द्वारा की जाती है इसलिए वह मालिक के निर्देश पर कार्य करता है तथा मालिक व ऐसे अभिकर्ता के मध्य संविदात्मक संबंध स्थापित होता है। वे एक दूसरे के प्रति अधिकार व उत्तरदायित्व रखते हैं। उन्हें उपअभिकर्त्ता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। डि बुशे बनाम आल्ट (1878) 8 चा० डि० 286 (310) सी० ए० के वाद में वादी ने चीन में स्थित एक जहाज न्यूनतम मूल्य निश्चित करके बिक्री करने के लिए क को अभिकर्ता मनोनीत किया। क मालिक की राय व जानकारी से ख को इस कार्य के लिए उपअभिकर्त्ता नियुक्त किया। ख ने उस वस्तु का खरीददार न मिलने के कारण स्वयं न्यूनतम मूल्य पर खरीद कर उसे ऊँचे लाभ पर विक्रय किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ख और मालिक के मध्य संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित होने के कारण वह प्राप्त लाभ के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा।
प्रश्न 22 एजेन्सी की स्थापना के तरीकों की व्याख्या कीजिए।
Explain modes of establishment of agencies.
उत्तर- एजेन्सी की स्थापना के तरीके स्वामी तथा अभिकर्ता के मध्य सृजित सम्बन्ध को अभिकरण (Agency) की संज्ञा दी गयी है। अभिकरण की स्थापना निम्न तरीके से हो सकती है –
(1) अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा एजेन्सी का सृजन हो सकता है।
(ii) विवक्षित तौर पर या आचरण द्वारा भी एजेन्सी की स्थापना होती है। यह दो प्रकार से हो सकती है
(क) विबन्ध द्वारा भी एजेन्सी की स्थापना होती है, तथा
(ख) पति-पत्नी के मध्य सहवास द्वारा।
(iii) आवश्यकता द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है।
(iv) अनुसमर्थन द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है। संविदा विधि की धारा 196 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे अभिकर्ता के रूप में नियोजित नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति के लिए परन्तु उस व्यक्ति की जानकारी तथा उस व्यक्ति के द्वारा अधिकार न दिये गये होने पर भी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जिसके लिए ऐसा कार्य किया गया है, यह विकल्प प्राप्त है कि या तो वह उसकी जानकारी तथा प्राधिकार के अभाव में किये गये कार्य को स्वीकार करे या अस्वीकार करे।
प्रश्न 23. अभिकरण को परिभाषित कर उसके अवयवों को इंगित कीजिए। क्या एक अवयस्क को अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है? Define Agency and point out its essentials. Can a minor be appointed as an agent?
उत्तर- अभिकरण- अभिकरण दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित एक सम्बन्ध है जिसमें एक व्यक्ति जिसे मालिक कहते हैं, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति देता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करता है।
ऐन्सन (Anson) महोदय के अनुसार, “यद्यपि सामान्य नियम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके किसी तीसरे व्यक्ति को न तो अधिकार दे सकता है और न तो उत्तरदायित्व अधिरोपित कर सकता है परन्तु नियोजन किये जाने पर यह उस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्षकार से विधिक सम्बन्ध स्थापित करे। इस उद्देश्य के नियोजन को अभिकरण कहते हैं। “
महेश चन्द्र वसु बनाम तिलकराम, ए० आई० आर० (1938) नागपुर 254-255 के वाद में अभिकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है “एक अभिकर्ता अपने स्वामी से, दूसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक सम्बन्ध उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है” वह शक्ति ही अभिकरण का मुख्य तत्व है।
यू० टी० आई० बनाम रविन्द्र कुमार शुक्ला, ए० आई० आर० (2005) एस० सी० 3528 के मामले में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (यू० टी० आई०) ने एक चेक पंजीकृत डाक द्वारा आदाता (Payee) को भेजा, परन्तु आदाता को यह चेक प्राप्त नहीं हुआ। आदादा यू टी० आई० के मध्य डाक से चेक भेजे जाने के सम्बन्ध में कोई संविदा नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पोस्ट ऑफिस यू० टी० आई० के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। चेक न पहुँचने का दायित्व पोस्ट ऑफिस का न होकर यू० टी० आई० का होगा।
अभिकरण के आवश्यक तत्व –
(i) अभिकरण के लिए दो व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध का वर्तमान रहना आवश्यक है।
(ii) एक व्यक्ति, जिसे स्वामी कहते हैं, वह अपनी सहमति दे कि दूसरा व्यक्त उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करे।
(iii) दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति देता है।
एक मान्य अभिकरण के निम्न मुख्य तत्व होते हैं-
(1) स्वामी संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
(ii) कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो कता है।
(iii) अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। (धारा 185)
अतः एक अवयस्क भी अभिकर्ता हो सकता है।
प्रश्न 24. प्रत्यापक अभिकर्ता कौन है?
Who is Del-Credre Agent?
उत्तर- प्रत्यापक अभिकर्ता (Del-Credre Agent) – यदि एक अभिकर्ता जो मालिक या स्वामी हो, यह प्रत्याभूति दे कि जिस व्यक्ति के साथ वह मालिक की और से सम्बन्ध बनाने हेतु संविदा कर रहा है यदि यह अन्य व्यक्ति से संविदा भंग करेगा तो उसको क्षतिपूर्ति हेतु अभिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तो ऐसे अभिकर्त्ता को प्रत्यापक अभिकर्त्ता (Del-Credre Agent) कहते हैं।
प्रश्न 25 अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण का क्या अर्थ है? व्याख्या करें। Explain agencies by ratification.
उत्तर- अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण (Agency by Ratification)- संविदा विधि की धारा 196 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे अभिकर्ता के रूप में नियोजित नहीं किया गया है. किसी व्यक्ति के लिए, परन्तु उस व्यक्ति की जानकारी तथा उस व्यक्ति के द्वारा अधिकार न दिये गये होने पर भी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जिसके लिए ऐसा कार्य किया गया है. यह विकल्प प्राप्त है कि या तो वह उसकी जानकारी तथा प्राधिकार के अभाव में किये गये कार्य को स्वीकार करे (अनुसमर्थन दे) या उस कार्य को अस्वीकार कर दे। यदि वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया गया है, उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है तो उस कार्य के परिणामों के लिए अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अधिकृत था परन्तु यदि यह व्यक्ति उस कार्य का अनुसमर्थन नहीं करता है तो वह कार्य उस पर बाध्यकारी नहीं होगा।
उक्त अनुसमर्थन (Ratification) अभिव्यक्त हो सकता है या विवक्षित। अभिव्यक्त अनुसमर्थन स्पष्टत: मौखिक या लिखित रूप से किया जाता है जबकि विवक्षित अनुसमर्थन पक्षकार के आचरण के आधार पर अनुमानित किया जाता है। (धारा 197) इस प्रकार स्वामी द्वारा अभिकर्ता के कार्य के अनुसमर्थन द्वारा भी अभिकरण का सृजन हो सकता है।
प्रश्न 26 अभिकरण का पर्यवसान।
Termination of Agency.
उत्तर- अभिकरण का पर्यवसान– अभिकरण की समाप्ति हो जाती है, यदि स्वामी द्वारा अभिकर्ता से प्राधिकार (अधिकार) का खण्डन कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है तथा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण का त्याग कर दिया जाता है, अभिकरण के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य की पूर्ति किया जाना जिसके लिए अभिकरण का सृजन हुआ था। इसके अलावा स्वामी या अभिकर्त्ता में से किसी एक की यदि मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है तथा मालिक या स्वामी यदि दिवालिया हो जाता है तो भी अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है। (धारा 201)
प्रश्न 27. उप-अभिकर्ता किसे कहते हैं?
Who is Sub- Agent?
उत्तर – उप अभिकर्त्ता – भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 191 उप- अभिकर्ता को परिभाषित करती है-उप अभिकर्त्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियन्त्रण के अधीन कार्य करता हो अर्थात् जो व्यक्ति अभिकर्त्ता द्वारा मालिक का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे उप-अभिकर्ता कहते हैं।
निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई अभिकर्ता अन्य व्यक्तियों से कार्य करवा सकता है अर्थात् उप अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है –
(क) जब व्यापारिक रूढ़ि के अनुसार उप अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती हो;
(ख) यदि उप-अभिकर्त्ता की नियुक्ति करना आवश्यक है;
(ग) मालिक की स्वीकृति मिल जाय; तथा
(घ) संकट काल में नियुक्ति की जा सकती है।
प्रश्न 28 अप्रकट स्वामी से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by undisclosed Principal?
उत्तर- अप्रकट नियोक्ता (स्वामी ) (धारा 231-232) – अप्रकट स्वामी का सिद्धान्त तब लागू होता है जब अभिकर्त्ता न तो मालिक का अस्तित्व बताता है न अपने अभिकर्ता होने की हैसियत इस परिस्थिति में अभिकर्त्ता, स्वामी तथा अन्य व्यक्ति के मध्य दायित्वों की क्या स्थिति है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि अभिकर्त्ता ने स्वामी को प्रकट न करके अपने नाम से संविदा की है तो अभिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा। उसके विरुद्ध तथा उसकी ओर से वाद चलाया जा सकता है। परन्तु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी जिसे अभिकर्त्ता ने प्रकट नहीं किया है, ऐसे अभिकर्त्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ संविदा करने पर हस्तक्षेप कर यह तर्क दे सकता है कि वह अप्रकट पक्षकार है। धारा 231 के अनुसार, जब अन्य व्यक्ति बिना इस जानकारी के संविदा करता है कि दूसरा व्यक्ति अभिकर्ता है तो अभिकर्ता का स्वामी संविदा को लागू करवाने की माँग कर सकता है।
अप्रकट स्वामी वह है जिसका अस्तित्व प्रकट किया जा सकता था लेकिन अभिकर्ता ने संविदा करते समय उसका नाम प्रकट नहीं किया है। यहाँ यह अनुमान किया जाता है कि अभिकर्ता स्वयं अपने नाम से संविदा करना चाहता था तब वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
जे० थामस एण्ड कम्पनी (जूट एण्ड गनीज) प्रा० लि० बनाम बंगाल जूट कम्पनी लिमिटेड, ए० आई० आर० 1979 कलकत्ता 20 के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अप्रकट स्वामी का अभिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
प्रश्न 29 अभिकर्ता के रूप में पत्नी पर संक्षिप्त नोट लिखें।
Write short note on the wife as Agent.
उत्तर- अभिकर्ता के रूप में पत्नी (Wife as an Agent)- पति तथा पत्नी साथ साथ रहते हैं अतः इनके मध्य विवक्षित अभिकरण (Constructive Agency) माना जाता है। जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है, उसे पति के नाम से घरेलू वस्तुएँ खरीदने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि कोई पत्नी अपने पति की गलतियों के कारण अपने पति से पृथक् रहती है तथा पति ने उसके भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है तो वह पत्नी आवश्यकता के आधार पर उसके द्वारा क्रय की गई वस्तु के लिए अपने पति को उत्तरदायी बना सकती है परन्तु अन्य कार्यों के सम्बन्ध में वह पति की अभिकर्त्ता नहीं होगी। परन्तु यदि पत्नी अपनी हो त्रुटियों के कारण पृथक् रहती है तो वह अपने पति की किसी भी प्रकार की अभिकत्ता नहीं होगी। केवल विवाह के तथ्य के आधार पर कोई पत्नी अपने पति की अभिकर्ता नहीं होगी परन्तु पत्नी को पति का अभिकर्त्ता होने के लिए एक घर की कल्पना की गई है तथा उस घर में पति-पत्नी दोनों रहते हों। पति तथा पत्नी के मध्य अभिकरण के लिए पति तथा पत्नी का एक घर में रहना (Cohabitation) आवश्यक है।
यदि पत्नी अपने जीवन स्तर से बाहर की वस्तु खरीदती है तो पति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे एक बाद में पत्नी ने सीज स्कीन का सिंगार केस, दस्ताने तथा सामान लिए। पति उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। पत्नी द्वारा
यदि पति अपनी पत्नी को आवश्यकताओं के लिए नकद रुपया देता है तो वह ली गई उधार की वस्तुओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यह स्मरणीय है कि पति अपनी पत्नी का अभिकर्ता नहीं होता। उसका प्राधिकार तभी उत्पन्न होता है जब ऐसा प्राधिकार पत्नी ने अभिव्यक्त रूप से दिया हो या पति द्वारा किये गये कार्यों का पत्नी द्वारा अनुमोदन किया जाय।
प्रश्न 30. अभिकर्ता एवं स्वतन्त्र ठेकेदार में अन्तर स्पष्ट करें। Distinguish between Agent and Independent contractor.
उत्तर – अभिकर्त्ता बनाम स्वतन्त्र ठेकेदार (Agent v. Independant Contractor)- स्वतन्त्र ठेकेदार वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट कार्य या उल्लिखित परिणाम उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेता है। यह मालिक के नियन्त्रण से स्वतन्त्र अपने ढंग से कार्य करता है
(1) अभिकर्ता तथा स्वतन्त्र ठेकेदार दोनों ही मालिक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।
(2) अभिकर्ता मालिक के नियन्त्रण में कार्य करता है किन्तु स्वतन्त्र ठेकेदार मालिक के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होता है।
(3) अभिकर्ता को मालिक समय-समय पर निर्देश दे सकता है कि कार्य किस प्रकार किया जाना है। ठेकेदार स्वतन्त्र रूप से अपने ढंग से अपने कार्य करता है, मालिक को केवल उल्लिखित परिणाम से मतलब होता है।
(4) अगर अभिकर्ता द्वारा कार्य अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया है तो उसके दुष्कृत्यों के लिए मालिक उत्तरदायी होगा जबकि स्वतन्त्र ठेकेदार के कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होता है।
(5) अभिकर्त्ता पारिश्रमिक के रूप में कमीशन लेता है। परन्तु ठेकेदार मालिक व ठेकेदार के मध्य तय की गई अभिनिश्चित धनराशि प्राप्त करता है।
प्रश्न 31. भागीदारी से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by Partnership?
उत्तर- भागीदारी की परिभाषा – भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 ” भागीदारी’ शब्द की परिभाषा देती है। धारा-4 में दी गई परिभाषा के अनुसार “भागीदारी उन व्यक्तियों के मध्य का सम्बन्ध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है, जो उन सब में से या उनमें से किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। “
वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर लो है व्यष्टितः भागीदार तथा सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वह फर्म का नाम कहलाता है।
भागीदारी अधिनियम की धारा 4 भागीदारी, भागीदार फर्म तथा फर्म के नाम की परिभाषा देता है। सरल शब्दों में कहें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र सहमति से आपस में मिल कर कोई कारबार (Business) चलाने का करार इस शर्त पर करते हैं कि वे उस कारबार के लाभ में अंश (हिस्सा) प्राप्त करेंगे तब भागीदारी अस्तित्व में आती है। भागीदारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि करार करने वाले सभी व्यक्ति कारबार का संचालन करें परन्तु उनमें यह करार हो सकता है कि कारबार का संचालन कुछ व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों की ओर से करेगा। इस करार को करने वाले व्यक्ति भागीदार कहलाते हैं तथा इस करार के फलस्वरूप संयुक्त कारबार के संचालन हेतु जो संस्था बनाई जाती है, उसे भागीदारी (Partnership) या फर्म (Firm) कहा जाता है।
प्रश्न 32 भागीदारी के आवश्यक तत्वों को विवेचित कीजिए।
Discuss the essential elements of Partnership.
उत्तर- भागीदारी के आवश्यक तत्व– भागीदारी के गठन के लिए निम्न आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए –
(1) भागीदारी के लिए कुछ व्यक्तियों के मध्य करार हो।
(2) इस करार का उद्देश्य किसी कारबार (Business) का संचालन हो ।
(3) करार के अन्तर्गत करार के पक्षकारों ने कारबार के फलस्वरूप होने वाले लाभ को आपस में वितरित करने के लिए सहमति की हो।
(4) करार के अन्तर्गत किए जाने वाले कारबार का संचालन करार के पक्षकारों में से एक या कई व्यक्तियों द्वारा उन सभी की ओर से किया जाय।
प्रश्न 33. भागीदारों के अधिकारों की चर्चा करें Discuss the rights of Partners.
उत्तर- भागीदार के अधिकार – भागीदारी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार – प्रत्येक भागीदार को व्यापार में हिस्सा लेने, भागीदारी का निर्णय बहुमत से कराने का अधिकार होता है। प्रत्येक भागीदार को यह अधिकार होता है कि यदि वह चाहे तो फर्म को लेखा पुस्तिकाओं की जाँच कर सकता है। भागीदारों को क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। व्यापार के संचालन में श्रमदान करने के लिए वेतन पाने का अधिकार, फर्म द्वारा अर्जित लाभ में समान रूप से अंश प्राप्त करने का अधिकार तथा अग्रिम धनराशि में 6 प्रतिशत की दर से व्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है।
प्रश्न 34. भागीदारी के विभिन्न प्रकार बतलाइये Explain the different kinds of partnership.
उत्तर– भागीदारी विभिन्न प्रकार की होती है-
(1) इच्छाधीन भागीदारी (धारा 7)
(2) विशिष्ट भागीदारी (धारा 8)
(3) निश्चित अवधि की भागीदारी
(4) सामान्य भागीदारी
(5) सीमित भागीदारी
(6) उपभागीदारी
(7) अवैध भागीदारी।
प्रश्न 35. विवक्षित प्राधिकार के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? What do you understand by principal of implied authority?
उत्तर- विवक्षित प्राधिकार के सिद्धान्त– सामान्य सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक भागीदार को जब तक वह भागीदारी में भागीदार बना रहता है, फर्म की ओर से कार्य करने का विवक्षित प्राधिकार होता है क्योंकि भागीदारी के संचालन में भागीदार को प्रतिदिन तथा प्रत्येक मामले में अधिकृत करना व्यवहार में सम्भव नहीं है अतः भागीदार को फर्म के लिए अभिकर्त्ता के रूप में सभी कार्य करने का विवक्षित अधिकार होता है। इसी को विवक्षित प्राधिकार का सिद्धान्त कहते हैं।
प्रश्न 36. “भागीदारी का निर्माण संविदा द्वारा होता है न कि प्रास्थिति द्वारा।” वर्णन कीजिए। Relationship of partnership arises from a contract and not from status. ” Discuss ?
उत्तर—भागीदारी का सम्बन्ध, संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं – भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 5 के अनुसार, भागीदारी का सम्बन्ध – संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं;
और विशेषकर हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य, जो उस हैसियत से कौटुम्बिक कारबार चलाते हैं, या बर्मी, बौद्ध, पति और पत्नी, जो उस हैसियत में कारवार चलाते हैं, ऐसे कारबार में भागीदार नहीं हैं।
अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, ‘भागीदारी’ ऐसे व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध है. जिन्होंने किसी ऐसे कारवार के लाभों में हिस्सा बँटाने का करार कर लिया हो जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं अथवा उन सबकी ओर से कार्यशील कोई एक व्यक्ति चलाता है। इस तरह भागीदारी के सृजन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच करार होना चाहिए और करार कारबार के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हो। भागीदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य का सम्बन्ध है जो करार द्वारा उद्भूत होता है। भागीदारी स्वेच्छापूर्वक संविदा द्वारा सृजित होती है और धारा 5 मुख्यतः भागीदारी की प्रकृति पर विशेष जोर देती है। इस धारा के अनुसार, भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं और विशेषकर हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य जो उस हैसियत में पारिवारिक कारवार चलाते हैं या वर्मी पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारबार चलाते हैं, भागीदार नहीं हैं। इस तरह जब हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य पारिवारिक कारोबार चलाते हैं तो उन्हें ऐसे कारवार में भागीदार नहीं माना जाता और भागीदारी अधिनियम उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होता है। वे हिन्दू विधि के अन्तर्गत शासित होते हैं।
प्रश्न 37. ‘फर्म’ से क्या तात्पर्य है? What do you mean by Firm?
उत्तर – फर्म (Firm )– भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में ‘फर्म’ का तात्पर्य बताया गया है – वे व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यक्तिगत रूप से भागीदार’ और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वह “फर्म नाम” कहलाता है।
कानून की दृष्टि में फर्म केवल भागीदारों का समूह है। “फर्म” विधिक व्यक्तित्व नहीं रखती है और न ही कोई ऐसा स्वत्व रखती है जो भागीदारों से भिन्न हो। फर्म का केवल इतना ही स्वत्व है कि यह भागीदारी के नाम से माध्यम से वर्णित है। भागीदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर फर्म का भी विघटन हो जाता है।
प्रश्न 38. (क) इच्छाधीन भागीदारी से आप क्या समझते हैं? What do you understand by partnership at will?
(ख) निष्क्रिय भागीदार से आप क्या समझते हैं? What do you understand by sleeping partner.
उत्तर ( क ) – इच्छाधीन भागीदारी (Partnership at will)—भागीदारी अधिनियम की धारा 7 इच्छाधीन भागीदारी ( Partnership at will) की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार इच्छाधीन भागीदारी से ऐसी भागीदारी का तात्पर्य है जिसके समयावधि या पर्यवसान (समापन) के सम्बन्ध में भागीदारों के मध्य कोई संविदा न हुई हो। ऐसी भागीदारी की समयावधि अनिश्चित होती है तथा यह भागीदारों की इच्छा तक जीवित रहती है।
इस प्रकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इच्छाधीन भागीदारी वह भागीदारी हैं जिसके लिए पक्षकारों ने यह संविदा नहीं की है कि यह भागीदारी कितनी अवधि तक अस्तित्व में रहेगी तथा उसके समापन की तिथि भी भागीदारों ने आपसी संविदा द्वारा निर्धारित नहीं की है।
इच्छाधीन भागीदारी में भागीदार सूचना देकर भागीदारी से पृथक हो सकते हैं। यदि संविदा में यह शर्त है कि भागीदार छः माह की पूर्व सूचना देकर भागीदारी से पृथक् हो सकते हैं तो यह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी नहीं होगी। इच्छाधीन भागीदारी में भागीदार जय चाहें अन्य भागीदार को सूचित कर भागीदारी से पृथक हो सकते हैं।
ए० वी० जोसेफ बनाम जोशी टी० जोसेफ, ए० आई० आर० (2012) केरल 56 के वाद में “इच्छाधीन भागीदारी” का आशय स्पष्ट किया गया है कि जब किसी भागीदारी संविदा में भागीदारों के मध्य उनके भागीदारी के सम्बन्ध में किसी भी अवधि का उपबन्ध न किया गया हो तो वह “इच्छाधीन भागीदारी” कही जाएगी।
उत्तर (ख ) – निष्क्रिय भागीदार (Sleeping Partner )— वह भागीदार जो फर्म के कारबार के संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेता अर्थात् भागीदारी में उसकी उपस्थिति का अहसास अन्य व्यक्तियों को नहीं होता ऐसा भागीदार जब तक भागीदारी में रहता है, फर्म के कार्यों के लिए अन्य भागीदारों के समान उत्तरदायी होता है। परन्तु जब वह फर्म से पृथक् होता है तो उसके लिए लोक सूचना (Public Notice) देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसकी फर्म में उपस्थिति की जानकारी ही आम जनता को नहीं होती। परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसे निष्क्रिय भागीदार की उपस्थिति की जानकारी रखते हों तो ऐसे व्यक्तियों को निष्क्रिय भागीदार के हटने की सूचना देनी आवश्यक है। चूँकि इस निष्क्रिय भागीदार की उपस्थिति का अहसास बाहरी व्यक्ति को नहीं होता अतः उसके द्वारा प्रदर्शन का प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न 39. व्यपदेशन (प्रदर्शन) के सिद्धांन्त की व्याख्या कीजिए। Explain the doctrine of holding out.
उत्तर– भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 28 में व्यपदेशन या प्रदर्शन (Holding out) ) के सिद्धान्त को सम्मिलित किया गया है। धारा 28 उपधारा (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने लिखित या मौखिक कथन (शब्दों) द्वारा या अपने आचरण द्वारा यह प्रदर्शन (व्यपदेशन करता है या जान-बूझकर प्रदर्शन किया जाने देता है कि वह किसी फर्म में भागीदार (partner) है तो ऐसी दशा में वह उस फर्म के भागीदार (Partner) के रूप में किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा जिसने किसी ऐसे प्रदर्शन (व्यपदेशन) पर विश्वास कर ऋण दिया है। यह अर्थहीन है कि वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का प्रदर्शन किया है। या जिसके भागीदार होने का प्रदर्शन किया गया है, उसे यह जानकारी है या नहीं कि वह प्रदर्शन ऐसे ऋण देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है।
उपरोक्त प्रदर्शन या व्यपदेशन के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण उदाहरण वाग बनाम कार्वर (Waugh v. Carver), [2H. Blacks 235] नामक वाद में मिलता है। इस वाद में एक व्यक्ति जो प्रमुख व्यापारी था, अपने व्यापार से निवृत्त होने के पश्चात् एक फर्म के भागीदारों के कहने पर उस फर्म का अवैतनिक अध्यक्ष हो गया। यद्यपि यह व्यापारी फर्म का वास्तविक भागीदार नहीं (Real Partner ) था परन्तु उसने फर्म के अवैतनिक अध्यक्ष पद को स्वीकार कर सामान्य जन में यह प्रदर्शन किया कि वह फर्म के कार्यकलाप में सक्रिय ही नहीं अपितु महत्वपूर्ण सहयोगी है। इस प्रदर्शन पर विश्वास करके एक व्यक्ति ने फर्म को ऋण दिया। ऋण देते समय ऋणदाता ने यह विश्वास किया कि वह भी फर्म का भागीदार था। न्यायालय ने व्यापारी को एक भागीदार की भाँति उत्तरदायी ठहराया।
मुख्य न्यायाधीश अय्यर ने प्रदर्शन के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि एक व्यक्ति अपना नाम भागीदार की हैसियत से प्रयोग होने दे तो वह संसार (आम जनता) के प्रति भागीदार हो जायेगा भले ही भागीदारी में संविदा के अधीन न तो वह धन या परिश्रम लगाता है या लाभ भी न प्राप्त करता हो क्योंकि ऐसा करना उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है जो इस प्रदर्शन पर विश्वास कर फर्म के साथ संव्यवहार करते हैं क्योंकि यह हो सकता है कि जिस ऋणदाता ने प्रदर्शन के आधार पर यह विश्वास करते हुए ऋण दिया कि वह फर्म का भागीदार है, यदि उसे वास्तविकता मालूम होती तो वह ऋण नहीं देता।
प्रश्न 40. दिवालिया भागीदार से आप क्या समझते हैं?What do you understand by Insolvent Partner?
उत्तर – दिवालिया भागीदार (Insolvent Partner ) – भागीदारी अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, यदि एक भागीदार दिवालिया निर्णीत किया जाता है, दिवालिया घोषित होने की तिथि से वह भागीदार नहीं रह जाता चाहे फर्म का विघटन हुआ हो या नहीं।
चूँकि एक दिवालिया भागीदार दिवालिया घोषित होने की तिथि से फर्म का भागीदार नहीं रह जाता अतः वह फर्म की ओर से फर्म के कारबार में भाग नहीं ले सकता। एक दिवालिया भागीदार प्रदर्शन के सिद्धान्त (Doctrine of holdig out) के आधार पर भी फर्म को आबद्ध नहीं कर सकता। दिवालिया होने की लोक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। एक दिवालिया भागीदार निवृत्त भागीदार माना जाता है जिसकी निवृत्ति की लोक सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है।
प्रश्न 41. भागीदारी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के कारोबार में अन्तर कीजिए। Differentiate between Partnership and Joint Hindu family business.
उत्तर- हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य जो पारिवारिक कारबार चलाते हैं, भागीदारी अधिनियम उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होता है। इसलिए सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण हिन्दू विधि के अनुसार होता है न कि भागीदारी अधिनियम के अनुसार।
भागीदारी तथा संयुक्त परिवार में अन्तर (Distinction between Partnership and Joint Family)
भागीदारी (Partnership)
(1) भागीदारी का निर्माण करार द्वारा होता है।
(2) भागीदारी में नया भागीदार सभी भागीदारों की सहमति के पश्चात् ही प्रविष्ट कराया जा सकता है।
(3) भागीदारी में एक भागीदार दूसरे भागीदार का अभिकर्ता होता है।
(4) भागीदारी का प्रत्येक सदस्य अपने सह-भागीदारों के साथ भागीदारी के सम्बन्ध में असीमित दायित्वों से बँध जाता है।
(5) भागीदारी के सम्बन्ध में प्रत्येक भागीदार का दायित्व व्यक्तिगत तथा संयुक्त-दोनों होता है।
संयुक्त परिवार (Joint Family)
(1) संयुक्त परिवार का निर्माण करार द्वारा न होकर पक्षकार की स्थिति (Status) के आधार पर होता है।
(2) संयुक्त परिवार में एक नवीन सदस्य अपने जन्म से ही सदस्यता ग्रहण कर लेता है। संयुक्त परिवार के सदस्य को संयुक्त सम्पत्ति में अधिकार जन्म से ही मिल जाता है।
(3) संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के अभिकर्ता (Agent) नहीं होते ।
(4) संयुक्त परिवार के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता।
(5) संयुक्त परिवार के सदस्यों का दायित्व व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता। उनका दायित्व संयुक्त सम्पत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है।
प्रश्न 42. ‘फर्म के कार्य’ को परिभाषित कीजिए। Define “Act of Firm”.
उत्तर- फर्म के कार्य (Act of Firm) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 को धारा 2 (क) के अनुसार फर्म का कार्य से फर्म के सब भागीदार या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता हो। अर्थात् “फर्म के कार्य” का आशय ऐसे कार्यों से है जो कि सभी भागीदारी के या किसी एक भागीदार या किसी अधिकर्ता के केवल वे कार्य फर्म के कार्य समझे जायेंगे जो फर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दायित्व उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार “फर्म के कार्य” को मात्र ऐसे कार्यों तक परिसीमित किया गया है जो पर-व्यक्तियों के सन्दर्भ में कोई दायित्व अथवा अधिकार उत्पन्न करते हों। अधिनियम के अध्याय 4 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें किसी भागीदार या अभिकर्ता का कार्य अधिकार या दायित्व उत्पन्न कर सकता है।
“फर्म के कार्य” की परिभाषा देना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी फर्म अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती। फर्म केवल अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से ही कार्य सम्पादित कर सकती है, जो इसके भागीदार होते हैं, फिर भी ऐसे अभिकर्ता भी माने जा सकते हैं जो भागीदार नहीं होते, क्योंकि किसी एजेण्ट या भागीदार का प्रत्येक कार्य “फर्म का कार्य” नहीं माना जा सकता। इस प्रकार यह एक तथ्यों पर आधारित होने वाला प्रश्न हो जाता है कि किसी अभिकर्ता या भागीदार का कौन-सा कार्य फर्म का कार्य माना जायेगा।
प्रश्न 43. फर्म से बाहर जाने वाले भागीदार के दायित्व ।Duties of an outgoing Partner.
उत्तर- फर्म से बाहर जाने वाले भागीदार का दायित्व – किसी प्रतिकूल संविदा या करार के अभाव में एक बाहर जाने वाला या निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निवृत्ति को तिथि से पूर्व किये गए फर्म के संव्यवहारों के लिए अन्य सह-भागीदारों की भाँति उत्तरदायी होगा।
परन्तु धारा 32 (2) में किए गये प्रावधान के अनुसार यदि सह भागीदार या अन्य व्यक्ति जिससे फर्म संव्यवहार करती है चाहे तो करार द्वारा एक (बाहर जाने वाले) भागीदार को अपने निवृत्ति से पूर्व के संव्यवहारों के दायित्व से मुक्त कर सकते हैं। यह करार विवक्षित भी हो सकता है तथा अन्य व्यक्ति को भागीदार के निवृत्त होने की जानकारी होने के पश्चात् अन्य व्यक्ति तथा पुनर्गठित फर्म के मध्य संव्यवहार के आचरण से अनुमानित किया जा सकेगा। परन्तु जो ऋणदाता नवीन व्यवस्था (फर्म के पुनर्गठन) को स्वीकार नहीं करते उनके प्रति निवृत्त होने वाले भागीदार का दायित्व बना रहता है। यदि निवृत्त होने वाला पक्षकार अपकृत्य या व्यापार चिन्ह का उल्लंघन का दोषी है तो उसका दायित्व उसकी फर्म से निवृत्ति के पश्चात् भी बना रहता है।
निवृत्ति के पश्चात् दायित्व – एक भागीदार के फर्म से निवृत्त होने पृथक् होने की लोक सूचना (Public notice) दी जानी आवश्यक है। ऐसी लोक सूचना (Public notice) फर्म द्वारा या निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा दी जानी आवश्यक है। यदि यह लोक सूचना नहीं दी गई है तो उसका प्रभाव यह होगा कि धारा 32 (2) के अनुसार वह भागीदार उनमें से किसी भागीदार द्वारा किये गए कार्य के लिए उत्तरदायी होगा जो उसकी निवृत्ति के पहले किये जाने पर फर्म का कार्य होता। परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह न जानते हुए फर्म से संव्यवहार करता है कि वह (निवृत्त) होने वाला भागीदार था तो निवृत्त होने वाला भागीदार उस अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
प्रश्न 44.एक पंजीकृत फर्म के लाभ। Advantages of a Registered Firm.
उत्तर- एक पंजीकृत फर्म के निम्नलिखित लाभ होते हैं-
(1) फर्म तथा उसके भागीदारों के मध्य वाद- भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या आपसी संविदा द्वारा प्राप्त अधिकारों को लागू कराने के लिए एक पंजीकृत फर्म का भागीदार फर्म के विरुद्ध या उसके वर्तमान या भूतपूर्व सह-भागीदारों के विरुद्ध वाद ला सकता है।
(2) फर्म तथा अन्य (बाहरी) पक्षकारों के मध्य वाद- धारा 69 (2) के अनुसार एक अपंजीकृत फर्म संविदा से उत्पन्न अधिकारों को लागू कराने हेतु किसी बाहरी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी वाद नहीं ला सकती जबकि पंजीकृत फर्म वाद ला सकती है।
उपरोक्त दो बातें मुजराई (set off) या संविदा से उत्पन्न अन्य अधिकारों को लागू कराने पर भी लागू होती हैं। उदाहरण के लिए एक बाहरी व्यक्ति एक अपंजीकृत फर्म के विरुद्ध कुछ धन वसूल करने के लिए वाद लाता है। इस परिस्थिति में फर्म यह नहीं कह सकती कि फर्म का उस व्यक्ति पर बकाया है, उसे मुजरा (Set off) कर लिया जाय।
प्रश्न 45. साझेदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। Discuss about the procedure of registration of a Partnership firm.
उत्तर- साझेदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया – भागीदारी अधिनियम की धारा 58 भागीदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करती है। भागीदारी फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन एक निर्धारित फार्म पर किया जाता है। इस निर्धारित फार्म (Prescribed Form) के माध्यम से निर्धारित (विहित Prescribed) शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। पंजीकरण के आवेदन पत्र में निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए-
(1) फर्म का नाम।
(2) स्थान या फर्म के व्यापार का मुख्य स्थान।
(3) ऐसे अन्य स्थानों का नाम जहाँ फर्म कारबार करती है।
(4) जिस तिथि पर प्रत्येक भागीदार ने फर्म में प्रवेश किया हो।
(5) फर्म के भागीदारों के नाम तथा स्थायी पते।
(6) फर्म की अस्तित्वावधि (फर्म कितने समय से अस्तित्व में है)।
उक्त सूचनाओं के साथ धारा 58 (2) के अनुसार आवेदन पत्र पर प्रत्येक भागीदार या उसके अभिकर्ता तथा यह प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है कि आवेदन पत्र में दिए गये सभी तथ्य उनकी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। यदि किसी भागीदार ने हस्ताक्षर नहीं किया है तो उस परिस्थिति में फर्म का पंजीकरण तभी संभव होगा जब उस हस्ताक्षर न करने वाले भागीदार का नाम फर्म से हटा दिया जाय।
भागीदारी अधिनियम की धारा 58 उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि फर्म के नाम के साथ क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस (सम्राज्ञी), एम्पायर, एम्पीरियल, किंग, क्वीन या रायल शब्द नहीं जुड़े होने चाहिए तथा जब तक राज्य सरकार ने लिखित आदेश के माध्यम से इन शब्दों के प्रयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान न की हो, फर्म के पंजीकरण के प्रार्थना पत्र में ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिनका तात्पर्य राज्य सरकार की अनुमति, संस्तुति या संरक्षकता का बोध होता हो।
उपरोक्त विवरण विहित (निर्धारित) प्रार्थना पत्र में भरकर विहित (Prescribed) शुल्क के साथ फमों के रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाना चाहिए-धारा 59 के अनुसार पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर यदि रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट है कि फर्म के पंजीकरण सम्बन्धी सभी अर्हताएँ तथा अन्य शर्तें पूरी हैं तो वह फर्मों का नाम फर्मों के रजिस्टर में चढ़ाकर फर्म का पंजीकरण कर लेगा तथा फर्म के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। यह प्रमाण-पत्र फर्म के पंजीकरण का साक्ष्य होगा।
प्रश्न 46. विशिष्ट भागीदारी एवं इच्छाधीन भागीदारी में अन्तर कीजिए। Differentiate between Particular Partnership and Partnership at will.
उत्तर- विशिष्ट भागीदारी एवं इच्छाधीन भागीदारी में अन्तर– भागीदारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी विशेष व्यापारिक कार्य (विशिष्ट प्रोद्यमों) अथवा उपक्रमों में भागीदार बनता है तब ऐसी भागीदारी को विशिष्ट भागीदारी कहते हैं।
जबकि धारा 7 के अनुसार जहाँ पर भागीदारी संविदा द्वारा भागीदारी की अवधि निश्चित न की गई हो या भागीदारी के पर्यवसाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वहाँ भागीदारी इच्छाधीन होगी।
प्रश्न 47. अवयस्क का लाभार्थी के रूप में भागीदारी में सम्मिलित होने को विवेचित कीजिए। Discuss the admission of minor as a beneficiary in a Partnership.
उत्तर- एक अवयस्क की भागीदारी के सम्बन्ध में विधिक स्थिति का वर्णन भागीदारी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत किया गया है। भागीदारी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अनुसार एक व्यक्ति जो उस पर लागू विधि के अन्तर्गत अवयस्क है, वह फर्म (भागीदारी) में भागीदार नहीं हो सकता परन्तु भागीदारी के सभी भागीदारों की सहमति से अवयस्क व्यक्ति को भागीदारी के फायदों (लाभों) के लिए भागीदारी में सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अनुसार एक व्यक्ति जिसने वयस्कता की वय (उम्र) प्राप्त नहीं की है अर्थात् जो अवयस्क है संविदा नहीं कर सकता यदि वह संविदा करता भी है तो उसके द्वारा की गई संविदा शून्य (निष्प्रभावी) होगी।
आयकर आयुक्त बनाम द्वारका दास खेतान एण्ड कम्पनी, ए० आई० आर० 1961 सु० को० 680 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एक अवयस्क व्यक्ति किसी भागीदारी (फर्म) में सम्पूर्ण भागीदार नहीं हो सकता। भागीदारी अधिनियम की धारा 30 सिर्फ यह प्रावधान करती है कि एक अवयस्क व्यक्ति को एक फर्म में सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किया जा सकता है परन्तु इसके लिए भी भागीदारी के सभी भागीदारों की सहमति आवश्यक है। यदि किसी भागीदारी विलेख (Partnership deed) में एक अवयस्क व्यक्ति को भागीदार बनाने की संविदा कर उपबन्ध किया जाता है तो ऐसा भागीदारी विलेख उस उपबन्ध या उस करार तक शून्य (निष्प्रभावी) होगा।
एक अवयस्क जिसे भागीदारी के सभी भागीदारों की सहमति से भागीदारी में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है, उसे यह अधिकार है कि-
अवयस्क को भागीदारी में की सम्पत्ति तथा भागीदारी के लाभ में अनुबन्धित अंश (Agreed Share) प्राप्त करने का अधिकार है। अपने अंश का पता लगाने के प्रयोजन से तथा अन्यथा अवयस्क को भागीदारी के लेखाओं (Accounts) की जाँच परीक्षण का तथा उसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 30 (2) परन्तु जब तक वह भागीदारी (फर्म) में बना रहता है, उसे भागीदारी की सम्पत्ति में अपना अंश तथा लाभ प्राप्त करने के लिए भागीदारों (Partners) के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। यदि वह वाद लाना चाहता है तो उसे भागीदारी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर भागीदारी त्यागनी होगी। यदि अवयस्क भागीदारी (फर्म) को छोड़ने के लिए सूचना (Notice) देता है तो अन्य भागीदारों में से या सभी भागीदारों द्वारा भागीदारी के विघटन के लिए वाद लाने के विकल्प के चुनाव (Elect) करने का अधिकार होगा तथा न्यायालय इस वाद को भागीदारी के विघटन के लिए वाद मान कर कार्यवाही कर सकती है।
प्रश्न 48. विक्रय की परिभाषा एवं विक्रय के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिये। Define sale and give essential elements of sale.
उत्तर-विक्रय (Sale)- किसी वस्तु का विक्रय एक प्रकार की संविदा है। इस संविदा में किसी निश्चित मूल्य पर एक पक्षकार किसी वस्तु का स्वामित्व दूसरे पक्षकार को अन्तरित करता है या अन्तरित करने का करार करता है।
वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 (जो पहले संविदा अधिनियम, 1872 का एक अंग था) की धारा 4 विक्रय की परिभाषा देती है। धारा 4 के अनुसार वस्तु के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें विक्रेता किसी वस्तु में सम्पत्ति का अन्तरण केता को एक मूल्य के लिए करता है या अन्तरित करने का करार करता है।
इस प्रकार विक्रय एक प्रकार की संविदा है जिसमें किसी मूल्य के लिए एक वस्तु (माल) में स्वामित्व वस्तु के स्वामी (विक्रेता) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (क्रेता) को अन्तरित किया जाता है या भविष्य में वस्तु का स्वामित्व अन्तरित करने का करार (Agreement) किया जाता है। विक्रम में संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं।
विक्रय के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Sale)
(1) उभयपक्षीय संविदा (Bilateral Contract);
(2) कोई मूल्य या कीमत जिसका धन के रूप में होना अनिवार्य (धन प्रतिफल) (Price-which should be in terms of money);
(3) वस्तु (माल) में स्वामित्व का अन्तरण या स्वामित्व के अन्तरण का करार;
(4) विक्रय की विषय-वस्तु (वस्तु माल Goods)।
प्रश्न 49. आश्वासन क्या है? What is Warranty?
उत्तर- आश्वासन (Warranty) – माल विक्रय अधिनियम की धारा 12 (3) में आश्वासन (Warranty) की परिभाषा दी गयी है।
आश्वासन संविदा के मुख्य प्रयोजन के साम्पाश्यिक यह अनुबन्ध (करार) है जिसके भंग या उल्लंघन होने से पक्षकार को क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है; परन्तु आश्वासन या वारण्टी के भंग या उल्लंघन से माल को अस्वीकृत करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् क्रेता संविदा को विखण्डित करके, माल वापस नहीं कर सकता तथा भुगतान की गई कीमत भी वसूल नहीं कर सकता। केवल उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न 50. (क) शर्त एवं वारण्टी में अन्तर कीजिए।Distinguish between condition and warranty.
(ख) हक के अन्तरण का क्या अर्थ है? इस सम्बन्ध में माल विक्रय अधिनियम में क्या प्रावधान है? What is meant by transfer of title? What are the provisions of Sales of Goods Act in this regard?
उत्तर (क)- शर्त एवं वारण्टी में अन्तर- शर्त माल विक्रय की एक महत्वपूर्ण तथा सारवान् अनुबन्ध होती है जबकि वारण्टी माल विक्रय की संविदा का साम्पाश्विक अनुबन्ध होता है। शर्त र्त का उल्लंघन व्यथित पक्षकार को माल वापस कर मूल्य वापस पाने का अधिकार देता है जबकि वारण्टी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार सिर्फ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। शर्त के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह संविदा को निरस्त कर सके जबकि वारण्टी के उल्लंघन से पीड़ित पक्षकार विक्रय की संविदा का विखण्डन नहीं कर सकता है, वह सिर्फ क्षतिपूर्ति की माँग कर सकता है।
उत्तर (ख) हक का अन्तरण (Transfer of title)- यह ‘नेमो डेट क्वाड नान हैबेट’ सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसा हक (स्वामित्व) एक व्यक्ति के पास है, वह उससे अच्छे हक (स्वामित्व) का अन्तरण नहीं कर सकता। उपरोक्त सिद्धान्त को माल विक्रय अधिनियम की धारा 27 में मान्य किया गया है।
नेमो डेट क्वाड नान हैबेट के सिद्धान्त को माल विक्रय अधिनियम की धारा 27 में अन्तर्निहित किया गया है।
धारा 27 इस प्रकार है- इस अधिनियम और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त (लागू) विधि के उपबन्धों के अध्यधीन (Subject to) यह है कि जहाँ कि माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जो उसका स्वामी नहीं है और जो स्वामी के प्राधिकार के अधीन या सम्मति से उसे नहीं बेचता, वहाँ क्रेता उस माल पर उस हक से, जो विक्रेता का था, बेहतर हक नहीं अर्जित कर सकता, जब तक कि माल का स्वामी विक्रेता के विक्रय प्राधिकार का प्रत्याख्यान करने से अपने आचरण द्वारा प्रवरित नहीं हो जाता।
धारा 27 में अन्तर्निहित नियम के अनुसार यदि एक व्यक्ति ऐसा माल बेचता है; जिसका वह स्वामी नहीं है या जिसे माल बेचने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी दशा में विक्रेता से क्रेता को कोई हक, अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा क्योंकि विक्रेता विक्रय की विषय-वस्तु में उस हक, अधिकार या स्वामित्व को अन्तरित नहीं कर सकता है जो हक, अधिकार या स्वामित्व माल के विक्रेता को स्वयं नहीं हो, परन्तु जिस व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक मूल्य देकर वस्तु क्रय की है, उसे भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
प्रश्न 51. क्रेता सावधान के नियमों की व्याख्या कीजिए। Describe rules of caveat emptor.
उत्तर- क्रेता सावधान का नियम – माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 क्रेता सावधान के नियम को प्रतिपादित करती है। ‘क्रेता सावधान’ के नियम के अनुसार यह प्रत्येक क्रेता का दायित्व है कि वह वस्तु क्रय करने से पूर्व सावधानीपूर्वक क्रय की जाने वाली वस्तुओं का परीक्षण कर यह देख ले कि जिस वस्तु का वह जिस प्रयोजन से क्रय कर रहा है वह वस्तु उस प्रयोजन के अनुरूप है या नहीं। प्रत्येक वस्तु निर्माता किसी खास प्रयोग के लिए किसी वस्तु को इस वारण्टी के साथ निर्मित करता है कि वह वस्तु उस प्रयोजन को पूरा करेगी परन्तु क्रेता किस प्रयोजन के लिए वस्तु क्रय कर रहा है यह उसके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता अतः उससे वस्तु क्रय करते समय इस बात के लिए सावधान रहने की अपेक्षा की जाती है कि वह वस्तु को देख-परख कर अपने प्रयोजन के अनुसार वस्तु को खरीदे।
क्रेता सावधान के नियम के अनुसार विक्रेता से किसी ऐसी वस्तु की आपूर्ति करने को बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो या उसमें कोई भी गुण विद्यमान हो। यह क्रेता का कर्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु देख-परख कर क्रय करें। क्रेता को किसी वस्तु के गुण तथा त्रुटियों से परिचित होना होगा जिसे वह क्रय करना चाहता है।
प्रश्न 52. ‘क्रेता सावधान’ नियम के किसी एक अपवाद की व्याख्या कीजिए। Explain any one exception to the rule of ‘caveat emptor’.
उत्तर- क्रेता सावधान नियम के अपवाद- (i) माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) क्रेता सावधान के नियम का प्रथम अपवाद प्रतिपादित करती है। इस उपधारा के अनुसार यदि क्रेता ने विक्रेता को किसी वस्तु के क्रय का अपना उद्देश्य प्रदर्शित कर दिया है तथा उसने विक्रेता के कौशल तथा जानकारी पर विश्वास किया है तो ऐसी दशा में यह विवक्षित शर्त (Implied Condition) रहती है कि वस्तु (माल) क्रेता के द्वारा बताये गये उद्देश्य के प्रयोजन के उपयुक्त हो तथा ऐसी परिस्थिति में क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा।
(ii) क्रेता सावधान के नियम का दूसरा अपवाद माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 (2) में अन्तर्निहित है। उपधारा (2) के अनुसार जहाँ विक्रेता द्वारा माल का क्रय वर्णनानुसार (by description) किया जाता है तथा विक्रेता उस वर्णन का व्यापार आमतौर पर करता है, वहाँ यह विवक्षित शर्त होगी कि माल वाणिज्यिक गुणवत्ता (Merchantable quality) का होगा। यह अर्थहीन है कि विक्रेता माल का निर्माता या उत्पादक है या नहीं। परन्तु यदि क्रेता माल की जाँच (परीक्षा) कर लेता है तो ऐसी त्रुटि के बारे में जो प्रत्यक्ष या प्रकट है कोई विवक्षित शर्त नहीं होगी अर्थात् यदि विक्रय किए जा रहे माल में त्रुटि प्रकट है या उसका पता आसानी से लग सकता था वहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू होगा तथा वह मामला अपवाद के अन्तर्गत नहीं आएगा।
प्रश्न 53. ‘नेयो हैट क्वाड नान हैबेट’ का सिद्धान्त क्या है? What is doctrine of “Nemo dat quod non habet”.
उत्तर- ‘नेमो बैट क्वाड नान हैबेट’ के सिद्धान्त को माल विक्रय अधिनियम की धारा 27 में अन्तर्निहित किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसा हक (स्वामित्व) एक व्यक्ति के पास है, वह उससे अच्छे हक का अंतरण नहीं कर सकता है।
सामान्य नियम यह है कि क्रेता विक्रेता के अधिकारों के अनुरूप हो माल में अधिकार प्राप्त करता है। जैसे एक विक्रेता, क्रेता को वही स्वत्व प्रदान कर सकता है जो स्वत्व उसे स्वयं माल में प्राप्त है। यदि माल के विक्रेता का माल के सम्बन्ध में स्वत्व दूषित है तो क्रेता का भी उस माल में दूषित स्वत्व रहेगा। इसके विपरीत यदि विक्रेता का माल में अच्छा स्वत्व है तो क्रेता का भी माल में अच्छा स्वत्व (Good title) रहेगा।
प्रश्न 54. अवक्रय करार से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Hire Purchase Agreement?
उत्तर- अवक्रय करार (Hire-Purchase Agreement) अवक्रय करार एक ऐसा करार है जिसके अधीन माल भाड़े पर दिया जाता है और अवक्रेता को यह विकल्प रहता है कि वह उस करार के निर्बन्धनों के अनुसार, उस माल को क्रय कर ले तथा इसके अधीन ऐसा करार भी है जिसके अधीन-
(i) माल के स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति को माल का कब्जा इस शर्त पर दिया जाता है कि वह व्यक्ति करार की गई रकम का संदाय कालिक किस्तों में कर दे, तथा
(ii) उन किस्तों में से अन्तिम किस्तों के संदाय पर ही सम्पत्ति उस व्यक्ति को संक्रान्त होनी है; तथा
(iii) उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सम्पत्ति के ऐसे संक्रान्त होने के पूर्व किसी भी समय करार को समाप्त कर दे।
प्रश्न 55. असंदत्त विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। Discuss the rights of an unpaid seller.
उत्तर- अदत्त विक्रेता वह विक्रेता है जिसे उसके द्वारा विक्रय की गई वस्तु के मूल्य का या तो पूर्णतः भुगतान नहीं हुआ है या मूल्य का किसी अंश (Part) का भुगतान होना शेष है। यदि किसी विक्रय की गई वस्तु का भुगतान लिखित परक्राम्य लिखत (Negotiable instrument) के माध्यम से हुआ है तो सामान्यतः विक्रेता असंदत्त (Unpaid) नहीं माना जाता परन्तु यदि माल के सम्प्रदान के पूर्व परक्राम्य लिखत (चेक, वचनपत्र आदि) का अनादर (dishonour) हो जाता है तो विक्रेता असंदत्त विक्रेता बन जाता है।
माल विक्रय अधिनियम की धारा 46 एक असंदत्त विक्रेता जिसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 45 में दी गई हैं, कुछ अधिकार प्रदान करती है भले ही विक्रय किए गए माल में सम्पत्ति (स्वत्व) क्रेता को चली गई हो। विधि के प्रभाव से एक असंदत्त (Unpaid) विक्रेता को निम्न अधिकार हैं –
(1) जब तक माल विक्रेता के कब्जे में है तब तक माल के मूल्य प्राप्त होने तक धारणाधिकार (Right of lien).
(2) यदि क्रेता (buyer) दिवालिया हो जाता है तो विक्रेता मूल्य के लिए माल को मार्ग में रोकने का अधिकार रखता है; तथा
(3) अधिनियम के प्रावधानों की सीमा में माल को पुनः बेचने का अधिकार।
असंदत्त विक्रेता का माल पर धारणाधिकार (Right of lien over goods) धारणाधिकार वह अधिकार है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति कुछ बकाया के भुगतान होने तक माल को अपने कब्जे में रख सकता है। अर्सदत्त विक्रेता को यह अधिकार है कि वह माल के मूल्य के प्राप्त होने तक माल को अपने पास रोके रख सकता है।
प्रश्न 56. विक्रय एवं विक्रय के करार में अन्तर बतलाइये।Distinguish between Sale and Agreement to sale.
उत्तर- विक्रय तथा विक्रय के करार में अन्तर (Distinction between Sale and Agreement to Sale)- विक्रय तथा विक्रय के करार के प्रभाव भिन्न होते हैं। अतः माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 (3) में इन दोनों के मध्य अन्तर स्पष्ट किया गया है। इस धारा के अनुसार जहाँ वस्तु से स्वत्व (Title) या सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को तुरन्त अन्तरित हो जाती है, वह संव्यवहार विक्रय कहलाता है परन्तु यदि क्रेता को स्वामित्व का अन्तरण किसी करार के अन्तर्गत निहित किसी शर्त के पूरा होने के पश्चात होना है, उस संव्यवहार को विक्रय का करार कहते हैं। विक्रय तथा विक्रय के करार में निम्न अन्तर हैं-
विक्रय (Sale)
(1) विक्रय में, माल में स्वामित्व का अन्तरण विक्रेता से क्रेता को तुरन्त विक्रय के समय ही हो जाता है।
(2) विक्रय में क्रेता विक्रय की विषय- वस्तु का स्वामी तुरन्त हो जाता है तथा वह स्वामित्व के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
(3) विक्रय में प्राप्त अधिकार को (Jus in rem) या सर्वबन्धी अधिकार कहते हैं।
(4) विक्रय हो जाने पर माल की हानि का जोखिम क्रेता पर होता है।
(5) विक्रय में यदि क्रेता मूल्य नहीं देता तो विक्रेता मूल्य प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है।
विक्रय का करार (Agreeement to Sale)
(1) विक्रय के करार में माल में स्वामित्व का अन्तरण तुरन्त न होकर करार में निर्धारित किसी शर्त के पूरा होने पर होता है।
(2) विक्रय के करार में क्रेता विषय- वस्तु (माल) का स्वामी तुरन्त नहीं होता परन्तु करार में निर्धारित शर्त के अनुसार स्वामित्व प्राप्त होता है।
(3) विक्रय के करार में प्राप्त अधिकार (Jus in Personam) व्यक्तिवादी अधिकार होता है।
(4) विक्रय के करार में जब तक विक्रय पूर्ण नहीं होता, माल में जोखिम विक्रय में ही निहित होता है।
(5) विक्रय के करार में विक्रेता मूल्य के लिए नहीं परन्तु संविदा भंग के लिए प्रतिकर के लिए वाद ला सकता है।
प्रश्न 57. नमूने द्वारा विक्रय को वर्णित कीजिए। Explain the sale by sample.
उत्तर – नमूने के अनुसार विक्रय (1) विक्रय की संविदा वहाँ नमूने के अनुसार विक्रय के लिए होती है जहाँ कि संविदा में तत्प्रभावी अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धन हो।
(2) नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है-
(क) कि माल का प्रपुंज क्वालिटी में नमूने के सदृश होगा;
(ख) कि क्रेता को माल के प्रपुंज नमूने से मिलान करने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त होगा;
(ग) कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त हो जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो।
नमूने के अनुसर विक्रय में निम्नलिखित विवक्षित शर्त रहती है-
(i) कि माल का प्रपुंज (Bulk), गुण, नमूने से सदृश होगा;
(ii) कि क्रेता को माल के प्रपुंज का नमूने से मिलान करने का युक्तियुक्त (Reasonable) अवसर प्राप्त होगा; तथा
(iii) कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त होगा, जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा से प्रकट नहीं होती है।
प्रश्न 58. माल से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Goods.
उत्तर- माल (Goods)- माल विक्रय संविदा की विषयवस्तु केवल “माल” ही हो सकता है। संविदा अधिनियम की धारा 2 (7) के अन्तर्गत “माल” का आशय “माल” से अनुयोज्य दावों (Actionable claims) और धन (Money) से भिन्न हर किस्म की जंगम (चल) सम्पत्ति अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत- स्टॉक, अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भागरूप ऐसी चीजें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक् किये जाने का करार किया गया हो। इस प्रकार खड़े पेड़ का भी विक्रय हो सकता है, यदि विक्रय के पूर्व या विक्रय की संविदा के अन्तर्गत उन्हें काटने या पृथक् करने का उपबन्ध किया गया हो। जैसे-जल, गैस, बिजली, जहाज, डिक्री, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेण्ट तथा कॉपीराइट भी माल माना जाता है। अनुयोज्य दावों व मुद्रा को माल के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। मुद्रा का आशय चालू मुद्रा (Current Money) से है। लेकिन ऐतिहासिक सिक्के, जो चलन में नहीं हैं, जैसे- मुगलकालीन, विक्टोरिया सिक्के इन्हें माल माना जाता है। इनका क्रय-विक्रय माल की तरह हो सकता है। विदेशी मुद्रा को भी माल माना जाता है। विट्ठलदास बनाम जगजीवन, ए० आई० आर० 1939 बाम्बे 84 के वाद में न्यायालय द्वारा कोर्ट की डिक्री को भी माल माना गया क्योंकि इनका भी क्रय-विक्रय हो सकता है।
प्रश्न 59. “सम्पत्ति के साथ जोखिम प्रथम दृष्टया हस्तान्तरित हो जाती है” व्याख्या कीजिए। “Risk prima facie passes with the Property.” Discuss.
उत्तर – सामान्य नियम यह है कि “जिस पक्षकार का स्वामित्व होता है, उसी का जोखिम भी होता है।” माल विक्रय की संविदा का उद्देश्य क्रेता को माल की सम्पत्ति का अन्तरण करना होता है। समस्या यह है कि किस समय विक्रेता से क्रेता को माल हस्तान्तरित हुआ माना जायेगा क्योंकि इसी आधार पर विक्रेता तथा क्रेता के अधिकार का निर्धारण होता है। माल के नष्ट या क्षतिग्रस्त होने के समय जो स्वामी रहता है, उसे ही जोखिम का वहन करना पड़ता है। जब करार के अन्तर्गत माल का स्वामित्व क्रेता को अन्तरित हो गया है और उसके बाद माल नष्ट होता है तो इस हानि को क्रेता वहन करेगा चाहे माल का परिदान क्रेता को किया गया हो या न किया गया हो। यदि माल के स्वामित्व का अन्तरण क्रेता को नहीं हुआ है तो माल के नष्ट होने की हानि विक्रेता को वहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार के स्वामित्व के साथ उसका जोखिम भी अन्तरित हो जाता है। संक्षेप में यह कि जिसके पास माल का मालिकाना हक, उसी के पास जोखिम रहेगी अर्थात् स्वामित्व के साथ जोखिम जुड़ी रहती है। इस बारे में नियम का उल्लेख माल विक्रय अधिनियम की धारा 26 में किया गया है-
धारा 26. जोखिम प्रथमदृष्ट्या सम्पत्ति के साथ संक्रान्त हो जाती है- माल तब तक विक्रेता की जोखिम पर रहता है जब तक कि उसमें की सम्पत्ति क्रेता को अन्तरित नहीं हो जाती, किन्तु जब उसमें की सम्पत्ति क्रेता को अन्तरित हो जाती है तब चाहे परिदान किया गया हो या नहीं, माल क्रेता की जोखिम पर रहता है।
किन्तु जहाँ कि परिदान क्रेता या विक्रेता के कसूर से विलम्बित होता है, वहाँ जोखिम कसूरवार पक्ष के ऊपर होता है। यह नियम प्रथमदृष्ट्या है क्योंकि सम्पत्ति का अन्तरण, जोखिम के अन्तरण की कोई परख नहीं है तथा पक्षकारों को अन्यथा करार करने से रोकने वाली कोई बात नहीं है। पक्षकार यह करार कर सकते हैं कि संक्रमण के समय जोखिम का अन्तरण नहीं होगा। उसके लिए किसी अन्य समय का करार कर सकते हैं।
प्रश्न 60. ‘अ’ तथा ‘ब’ ने भागीदारी में एक टैक्सी कार खरीदी। एक साल बाद ‘अ’ ने ‘ब’ को बताये बगैर टैक्सी बेच दी। ‘ब’ अपना भाग प्राप्त करने के लिए ‘अ’ पर वाद लाया। ‘अ’ ने अपने बचाव में यह कहा कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवायी गयी थी। क्या ‘ब’ अपना भाग प्राप्त कर सकेगा, कारण सहित बताइए। ‘A’ and ‘B’ purchased a taxi car in partnership. After one year without the consent of ‘B’, ‘A’ sold the taxi car. “B’ filed a suit against ‘A; for his share. ‘A’ took defence of non-registration of firm. Will ‘B’ able to get share. Discuss with reason.
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (3) एवं 69 (4) से सम्बन्धित है जो धारा 69 (1) एवं 69 (2) का अपवाद है। फर्म के अपंजीकृत होने की दशा में भी निम्नलिखित परिस्थितियों में वाद चलाया जा सकता है-
(1) अपंजीकृत फर्म के विघटन के लिए भागीदार वाद संस्थित कर सकते हैं।
(2) यदि कोई अपंजीकृत फर्म विघटित होती है तो उसके लेखा अर्थात् हिसाब जानने के लिए भागीदार द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है।
(3) यदि अपंजीकृत फर्म का विघटन हो गया है तो इसके भागीदार फर्म की सम्पत्ति को वसूल करने के लिए वाद चला सकते हैं।
प्रस्तुत समस्या में ‘अ’ तथा ‘ब’ ने भागीदारी में एक टैक्सी खरीदी थी जिसे एक वर्ष बाद ‘अ’ने ‘ब’ को बताये बिना बेच दी, अतः, फर्म विघटित हो गयी। ‘ब’ ने अपना भाग प्राप्त करने के लिए ‘अ’ पर वाद दायर किया जो सही था।’ अ’ द्वारा यह प्रतिवाद करना कि फर्म का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, इसमें वह सफल नहीं होगा।
अतः, ‘ब’ अपना भाग प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है।
पी० के० वेंकटेश्वलू बनाम सी० लक्ष्मी नरसिम्हाराव, ए० आई० आर० (2002) ए० पी० 62 के मामले में अभिमत व्यक्त किया गया कि भागीदार अपंजीकृत फर्म के विघटन के लिए वाद संस्थित कर सकता है और उसे इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि फर्म पंजीकृत नहीं है।
प्रश्न 61. ‘ब’ को पहली मार्च को 5,000 रुपये उधार देने की संविदा ‘स’ करता है। ‘अ’ उस ऋण के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति करता है। ‘स’ 5,000 रुपये ‘ब’ को पहली जनवरी को दे देता है। क्या ‘अ’ अपने दायित्व से उन्मोचित हो गया? यदि हाँ तो क्यों? स्पष्ट कीजिए। ‘C’ agrees to give loan to ‘B’ or Rs. 5,000 on 1st March and contracts. ‘A’ took guarantee for refund of said debt. ‘C’ gives Rs. 5,000 to ‘B’ on 1st January. Does ‘A’ discharge from his liability? If yes why? Clarify.
उत्तर- दी गयी समस्या संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 133 के दृष्टान्त (ड) पर आधारित है। धारा 133 यह प्रावधानित करती है कि “यदि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में कोई सारभूत परिवर्तन कर देता हो तो उसके पश्चात् होने वाले संव्यवहारों के लिए प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात् प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। प्रतिभू को दायित्व से उन्मुक्ति देने के लिए आवश्यक है कि संविदा का परिवर्तन उसकी स्थिति को सारतः प्रभावित करे। [प्रागदास बनाम धनीराम (1931)]।
प्रस्तुत समस्या में ‘अ’ (प्रतिभू) की सहमति के बिना ‘स’ (ऋणदाता) संविदा में सारभूत परिवर्तन कर देता है। ‘स’ ऋण ‘ब’ को पहली मार्च को न देकर पहली जनवरी को ही दे देता है। अतः, ऐसे संव्यवहारों के लिए प्रतिभू (अ) जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात् प्रतिभू का उन्मोचन हो गया।