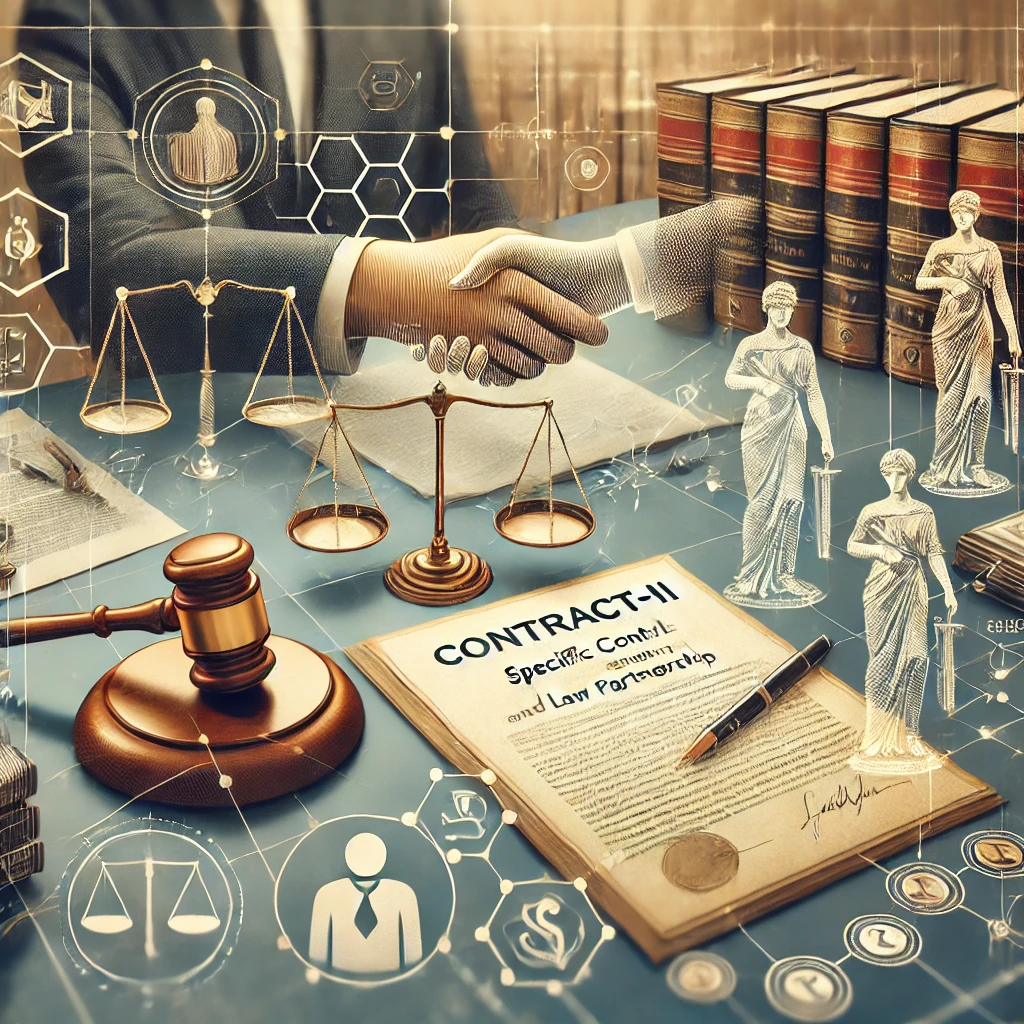-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
क्षतिपूर्ति (Indemnity)
(धाराएँ 124 एवं 125 )
प्रश्न 1. क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रतिग्रहीता अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता हुआ, प्रतिज्ञाकर्ता से कौन-सी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है? Define the Contract of Indemnity. What damages the promisee in contract of Indemnity, acting within scope of his authority, is entitled to recover from the promisor.
उत्तर- क्षतिपूर्ति की संविदा (Contract of Indemnity) — भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है कि “वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, ‘क्षतिपूर्ति की संविदा” कहलाती है। इस प्रकार इस संविदा में, पक्षकारों के बीच एक सीधा सम्बन्ध स्थापित होता है। एक पक्षकार जो बचाने या क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा करता है उसे क्षतिपूर्तिदाता (Indemnifier) तथा दूसरा पक्षकार जिसको क्षतिपूर्ति की जाती है, को क्षतिपूर्तिधारी (Indemnity holder) कहते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षतिपूर्तिधारी को अपने आचरण से, या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचायेगा। जैसे-‘राम’, ‘श्याम’ को उस कार्यवाही से हुई हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है जो कार्यवाही ‘वन्दना’, ‘श्याम’ के विरुद्ध 2,000 रुपये के सम्बन्ध में चलायेगा। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। अर्थात् इस परिभाषा से स्पष्ट है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल मनुष्य के आचरण से उत्पन्न होने वाली क्षति ही क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। क्षतिपूर्ति की संविदा में मनुष्य के आचरण से भिन्न किसी घटना से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति प्रतिज्ञा (वचन) नहीं होती। इस प्रकार बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती। बीमा की संविदा (जीवन बीमा को छोड़कर) समाश्रित संविदा होती है। यद्यपि क्षतिपूर्ति की संविदा विवक्षित हो सकती है। इस प्रश्न पर धारा 124 मौन है, परन्तु प्रिवी काउन्सिल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम भारत संघ, (1938) के बाद में यह मत व्यक्त किया कि क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त तथा विवक्षित दोनों हो सकती है ।
अंग्रेजी विधि इस मामले में भारतीय विधि से अधिक व्यापक है। अंग्रेजी विधि में किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति की पूर्ति की संविदा क्षतिपूर्ति को संविदा होगी। चाहे वह मनुष्य के आचरण के कारण हो या आग, वर्षा या किसी अन्य घटना से परन्तु भारतीय विधि धारा 124 से शासित होती है जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा में अपने या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली क्षति की पूर्ति करने की संविदा होती है अत: भारतीय विधि सीमित है।
भारतीय विधि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित बाद विश्वनाथ बनाम ओरिएण्टाल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ए० आई० आर० (2002) दिल्ली 336 में एक मोटर गाड़ी के लिए 1,00,000 रुपये की बीमा पॉलिसी की गई थी। मोटर गाड़ी के चोरी हो जाने के फलस्वरूप वादी को हानि हुई। बीमाकर्ता का यह तर्क कि उसका दायित्व मोटर के बाजार मूल्य तक सीमित था, न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
क्षतिपूर्तिधारी, अपने प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करते हुए क्षतिपूर्तिदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) से कौन-सी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है? भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रतिज्ञाग्रहीता अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता हुआ प्रतिज्ञाकर्ता से निम्न क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है-
(1) क्षतिपूर्तिधारी (प्रतिज्ञाता) यदि किसी बात से सम्बन्धित चलाये गये बाद में यदि कोई नुकसानी या क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया गया है जिसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की संविदा की गई है तो वह क्षतिपूर्तिदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) से नुकसानी या प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई राशि को प्राप्त कर सकता है।
(2) यदि प्रतिज्ञाग्रहीता (क्षतिपूर्तिधारी) किसी बाद की लागत या खर्च भी प्रतिज्ञादा क्षतिपूर्तिदाता) से प्राप्त कर सकता है, यदि क्षतिपूर्तिदाता (प्रतिदाता) में क्षतिपूर्तिधारी (प्रतिज्ञाग्रहीता) को बाद चलाने या बचाव करने हेतु अधिकृत किया हो। यदि वाद के संचालन या बचाव करने में प्रतिज्ञादाता (क्षतिपूर्तिदाता) के आदेशों का उल्लंघन न किया हो तथा क्षतिपूर्तिधारी ने एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की भाँति कार्य किया है।
(3) प्रतिज्ञाग्रहीता (क्षतिपूर्तिधारी) वह धनराशि प्रतिज्ञाकर्ता (क्षतिपूर्तिदाता) से प्राप्त कर सकता है जो उसने मुकदमे के समझौते के अन्तर्गत भुगतान किया है। यदि यह समझौता प्रतिज्ञादाता (क्षतिपूर्तिदाता) के आदेशों के उल्लंघन में नहीं किया गया है तथा एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी प्रश्नगत परिस्थितियों में इसी प्रकार का समझौता करता यदि वह समझ करने हेतु अधिकृत किया गया होता।
क्षतिपूर्तिग्रहीता क्षतिपूर्ति को कम कर सकता है? इस बिन्दु पर भारतीय न्यायालयों में मतभेद है। लाहौर और नागपुर उच्च न्यायालयों के अनुसार, क्षतिपूर्तिधारी तब तक क्षतिपूर्ति की माँग नहीं कर सकता जब तक उसे वास्तव में क्षति न हुई हो। परन्तु बम्बई, कलकत्ता तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के अनुसार क्षतिपूर्तिधारी वास्तव में क्षति होने से पूर्व क्षतिपूर्ति की माँग कर सकता है। विधि आयोग ने अपने 13वें प्रतिवेदन में इस मत का समर्थन किया है कि क्षतिपूर्तिधारी क्षति होने से पूर्व भी क्षतिपूर्ति की माँग कर सकता है। विधि आयोग ने विधायिका द्वारा इसी अनुरूप का संशोधन करने की संस्तुति की है।
प्रश्न 2. क्षतिपूर्ति की संविदा की प्रकृति का उल्लेख करते हुए बतायें कि क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व का प्रारम्भ किस समय होता है? When does liability of Indemnifier begin by describing the nature of Contract of Indemnity?
उत्तर – जहाँ तक क्षतिपूर्ति को संविदा की प्रकृति की बात है, यह संविदा अभिव्यक्त या उपलक्षित हो सकती है। कभी-कभी पक्षकारों का आचरण ही पर्याप्त होता है, जैसा कि बाद डगडेल बनाम लोवरिंग, (1875) 10 सी० पी० 196 में स्पष्ट किया गया है। प्रतिवादी एवं एक कम्पनी कुछ ट्रकों के दावेदार थे जो वादी के कब्जे में थीं। लेकिन स्वामित्व किसी का नहीं सिद्ध हो सका था। प्रतिवादी द्वारा वादी से ट्रक की माँग की गई। वादी इस आधार पर देने के लिए तैयार हुआ कि प्रतिवादी द्वारा एक क्षतिपूर्ति बाण्ड दिया जाये। प्रतिवादी की तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर भी वादी ने प्रतिवादी को ट्रक दिया। तत्पश्चात् के० पी० कम्पनी के द्वारा स्वामित्व सिद्ध किये जाने पर वादी उस ट्रक का मूल्य देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अतः वादी उस उत्तरदायित्व (हानि) की पूर्ति प्रतिवादी से प्राप्त कर सकता है। यद्यपि कि प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से कोई प्रतिज्ञा नहीं किया था। लेकिन ट्रक को स्वीकार करके आचरण द्वारा सिद्ध किया कि वह सहमत था, जिसके फलस्वरूप संविदा का प्रादुर्भाव हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड, (1938) 175, आई० सी० 327 (पी० सी०) के बाद में अभिव्यक्त प्रतिज्ञा के विषय में स्पष्ट किया गया है। एक बैंक को गलत पृष्ठांकनयुक्त ऋण-पत्र जारी किया गया जिसे उसने सद्भावना से प्राप्त किया। पृष्ठांकिती का नाम बदलने के लिए उसे लोक ऋण विभाग को भेज दिया गया। ऋणपत्र के वास्तविक स्वामी ने सरकार से दूसरे व्यक्ति का नाम बदलने के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली तथा सरकार ने बैंक से क्षतिपूर्ति प्राप्त किया। अन्य वाद इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। एक बैंक के आग्रह पर कारपोरेशन ने कुछ अंशों का अन्तरण पंजीकृत किया जो जाली सिद्ध हुआ। न्यायालय द्वारा बैंक को दायी ठहराया गया।
क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व का प्रारम्भ (Commencement of liability)— क्षतिपूर्तिदाता के दायित्व का प्रारम्भ किस समय होता है इस सम्बन्ध में न्यायालयों के मतों में विभिन्नता पायी जाती है। श्याम लाल बनाम अब्दुल सलार, ए० आई० आर० 1931, इलाहाबाद 754 तथा चुन्नी भाई पटेल बनाम माथाभाई, ए० आई० आर० 1944, पटना 185 जैसे वादों में उच्च न्यायालयों के अनुसार जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी क्षति देने के लिए उत्तरदायी मान लिया जाय, वैसे ही क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान के लिए माँग कर सकता है, परन्तु कुछ उच्च न्यायालयों के मतानुसार वास्तविक हानि हुए बिना अर्थात् हानि की पूर्ति किये बिना क्षतिपूर्तिधारी क्षति प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रायः दोनों पक्षकार आपस में यह तय करते हैं कि एक दूसरे पक्षकार को होने वाली हानि की पूर्ति करेगा, बशर्ते कि वह उसके कथनानुसार कार्य करे।
गजानन मोरेश्वर बनाम मदन मोरेश्वर, ए० आई० आर० (1942) बाम्बे के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ‘जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान के लिए धन की माँग कर सकता है।”
सुजिर गणेश नायक एण्ड कम्पनी, क्विलोन बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, (1996) के मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बीमा कम्पनी कर्मकारों द्वारा जानबूझकर की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप कम्पनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है।
प्रत्याभूति (Guarantee)
(धाराएँ 126 एवं 147)
प्रश्न 3. प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं? प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं? यह किस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा से भिन है? विवेचना कीजिए। What do you understand by Contract of Guarantee? What are the essential elements of Contract of Guarantee? In what respect is it different from a Contract of Indemnity? Discuss.
उत्तर- प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Guarantee)- संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126 प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू (Surety), मूल ऋणी (Principal) Debtor) तथा लेनदार (Creditor) की परिभाषा देती है। प्रत्याभूति की संविदा से तात्पर्य एक ऐसी संविदा से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (चूक) व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा (वचन) के पालन या उसके दायित्वों को पूरा करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है ‘प्रतिभू’ कहलाता है, वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है. “मूलऋणी” कहलाता है और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, ‘लेनदार’ कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी अर्थात् यह एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायित्व लेता है।
‘क’, ‘ख’ से 50,000 रुपया उधार लेता है तथा उसे तीन वर्ष के भीतर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। ‘ग’, ‘ख’ को यह वचन देता है कि यदि ‘क’, तीन वर्ष के अन्दर 50,000 रुपया वापस नहीं करता है तो वह 50,000 रुपया वापस करेगा। यह ‘ग’ तथा ‘ख’ के मध्य हुई संविदा प्रत्याभूति की संविदा हुई। जो व्यक्ति प्रत्याभूति (Guarantee) देता है उसे प्रतिभु तथा जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वह मूल ऋणी (Principal) Debtor) कहा जाता है। जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है उसे लेनदार (Creditor) कहते हैं।
जिस संविदा में स्वतन्त्र उत्तरदायित्व वर्तमान है, वह प्रत्याभूति की संविदा नहीं होती है, जैसे- ‘क’ दुकानदार से कहता है कि ‘ख’ को कुछ सामान दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मूल्य आपको मिल जायेगा। यह एक स्वतन्त्र प्रतिज्ञा है न कि प्रत्याभूति टेलर बनाम ली (1928) सुप्रीम कोर्ट ऑफ नार्थ केरोलिना के एक अमेरिकी बाद में एक मकान मालिक अपने किरायेदार के साथ वादी की दुकान पर गया और कहा, “श्री पारकर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे जो माल चाहें उन्हें दे दीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता है कि भुगतान मिल जायेगा।” न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह एक स्वतन्त्र प्रतिज्ञा है। अतः यह प्रत्याभूति की संविदा नहीं मानी गयी।
इण्डियन ओवरसीज बैंक बनाम एस० एन० जी० कास्ट्रोराइट प्राइवेट लिमिटेड, ए० आई० आर० (2002) दिल्ली 309 के बाद में यह आश्वासन दिया गया कि ऋणी अपना ऋण चुका सकता है। न्यायालय ने इसे प्रत्याभूति की संविदा नहीं माना।
मेसर्स यूनाइटेड ब्रेबरीज लिए बनाम कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेन्ट एण्ड डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि० एण्ड अदर्स, ए० आई० आर० (2012) कर्नाटक 65 संधारी कम्पनी द्वारा अपने एसोसियेट कम्पनी के पक्ष में ‘लेटर ऑफ काम्फर्ट’ जारी किया गया कि कम्पनी, वित्तीय व संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हैं। लेटर ऑफ काम्फर्ट सिफारिशी पत्र था, इसे प्रत्याभूति नहीं माना जायेगा।
प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व (Essential elements of contract of guarantee) – एक वैध प्रत्याभूति की संविदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-
(1) पक्षकार – प्रत्याभूति की संविदा के तीन पक्षकार होते हैं-
(i) प्रतिभूः
(ii) मूल ऋणी तथा
(iii) लेनदार (ऋणदाता)।
यहाँ मूल ऋणी तथा ऋणदाता के मध्य संविदा होती है, जिसके अन्तर्गत मूल ऋणी किसी प्रतिज्ञा या दायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। तत्पश्चात् प्रतिभू व लेनदार (ऋणदाता) के मध्य संविदा होती है जिसके अन्तर्गत प्रतिभू यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि मूल ऋणी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने या अपने दायित्व का निर्वहन करने में चूक करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा। एक संविदा प्रतिभू व मूल ऋणी के मध्य होती है जिसके द्वारा मूल ऋणी, प्रतिभू को क्षतिपूर्ति करने की विवक्षित प्रतिज्ञा करता है।
(2) मूल ऋण – प्रत्याभूति को संविदा का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक – कि मूल ऋण न हो, क्योंकि मूल ऋण को सुरक्षित करना ही प्रत्याभूति को संविदा का मुख्य उद्देश्य है। अतः ऋण का वैध व प्रवर्तनीय होना आवश्यक है।
काउट्स एण्ड कम्पनी बनाम ब्राउन लेकी, (1947) 1 के० बी० 106 के बाद में प्रश्न यह था कि जब किसी अवयस्क के ऋण के लिए प्रत्याभूति दी जाये तो यदि अवयस्क का ऋण शून्य होता है तो क्या प्रतिभू दायी होगा? इस बाद में निर्णीत किया गया कि ऐसी स्थिति में प्रतिभू दायी नहीं होना चाहिए।
(3) दायित्व – दायित्व से आशय विधि द्वारा प्रवर्तनीय दायित्व से है। यदि दायित्व न हो तो प्रत्याभूति की संविदा ही नहीं होती। मंजू महादेव बनाम शिवप्पा, 42 बाम्बे 444 के बाद में बम्बई हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि कालावरोधित ऋण (Time-barred debt) के लिए प्रतिभू दायी नहीं है क्योंकि मूल ऋणी दायी नहीं होता। चूंकि मुख्य दायित्व मूल ऋणी का है, तत्पश्चात् उसकी असफलता पर गौण दायित्व प्रतिभू पर होता है। यदि मुख्य ऋणी किन्हीं परिस्थितियों में उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो जाता है तो प्रतिभू भी उन्मुक्त मान लिया जाता है।
(4) मौखिक या लिखित (धारा 126 ) – प्रत्याभूति की संविदा का लिखित होना जरूरी नहीं है। यह लिखित या मौखिक हो सकती है।
एक्सन स्ट्रेन्थ लिमिटेड बनाम इण्टरनेशनल ग्लास इंजीनियरिंग इन ग्लीन एस० पी० ए०, (2003) आल० ई० आर० 615 (एच० एल०) के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति मौखिक प्रत्याभूति के अन्तर्गत दायी हो सकता है यदि उसके आचरण के कारण या व्यपदेशनों के कारण, उसे यह कहने नहीं दिया जायेगा कि प्रत्याभूति मौखिक थी।
(5) मिथ्याव्यपदेशन या तात्विक तथ्य के छिपावट द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त न की गई हो (धारा 142-143) – यदि कोई प्रत्याभूति लेनदार या उसकी जानकारी या अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग के बारे में असत्य कथन ( मिथ्या व्यपदेशन) करके या छिपाव करके प्राप्त की गई है तो ऐसी प्रत्याभूति की संविदा अवैध होगी। धारा 143 के अनुसार प्रत्याभूति उस समय भी अवैध होगी जबकि सारवान परिस्थितियों के बारे में लेनदार मौन रहता है तथा प्रत्याभूति इस चुप्पी के फलस्वरूप प्राप्त की गई है।
जैसे ‘क’, ‘ख’ (एक नौकर) की ईमानदारी के बारे में प्रत्याभूति देता है जिस व्यक्ति को वह ‘ख’ के बारे में प्रत्याभूति देता है वह ‘ख’ को पहले बेईमानी के कारण नौकरी से निकाल चुका है परन्तु नियोजक (लेनदार) इस तथ्य को ‘क’ (प्रतिभू) को नहीं बताता। यह प्रत्याभूति की संविदा मान्य नहीं होगी क्योंकि, यह छिपाव द्वारा प्राप्त थी।
(6) प्रतिफल – प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक होता है परन्तु – लेनदार और प्रतिभू के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है।
प्रकाशवती जैन बनाम पंजाब इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, ए० आई० आर० (2012) पी० एण्ड एच0 13 के बाद में मूल ऋणी के लाभ के लिए प्रतिभू द्वारा दी गई। कोलेटरल सिक्योरिटी पर्याप्त प्रतिफल माना गया है।
क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर –
क्षतिपूर्ति (Guarantee)
(1) प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं।
(2) प्रत्याभूति की संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है ।
(3) प्रत्याभूति ( गारण्टी) मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है।
(4) अंग्रेजी विधि में ऐसी संविदा मात्र लिखित रूप में ही होती है जबकि भारत में ऐसी कोई शर्त नहीं है।
(5) प्रत्याभूति की संविदा में प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का होता है । प्रतिभू का दायित्व द्वितीय होता है।
(6) प्रतिभू मूल ऋणी का ऋण चुका कर मूल ऋणी पर रकम वसूल करने का दावा कर सकता है।
प्रत्याभूति (Indemnity)
(1) इसमें दो पक्षकार होते हैं।
(2) यह मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है।
(3) यह संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं होती है।
(4) मौखिक एवं लिखित दोनों तरह की हो सकती है।
(5) ऐसी संविदा में क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला ही पूर्णरूप से जिम्मेदार होता है ।
(6) इस संविदा के अन्तर्गत क्षतिपूरक किसी से भी रकम वसूल नहीं कर सकता है।
प्रश्न 4. प्रत्याभूति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या एक प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है? Enumerate the kinds of Guarantee. Is consideration necessary for a contract of guarantee?
उत्तर- प्रत्याभूति के प्रकार- प्रत्याभूति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है—
(1) विशिष्ट प्रत्याभूति तथा
(2) चलत प्रत्याभूति ।
(1) विशिष्ट प्रत्याभूति (Specific Guarantee) – भविष्य में पालन की जाने की प्रत्याभूति या तो एक ऋण या ऋण की निश्चित राशि तक अर्थात् एक संव्यवहार के लिए होती है और उसके पूर्ण होते ही समाप्त हो जाती है उसे विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। जैसे- ‘हर्ष’, ‘शिवांश’ को यह वचन देता है कि यदि वह (शिवांश) ‘ऋषभ’ को 10,000 रुपये ऋण के रूप में देगा तो यदि ‘ऋषभ’ द्वारा ऋण वापस करने में चूक की जाती है तो उक्त स्थिति में ऋण की राशि वह (हर्ष) ‘शिवांश’ को वापस कर देगा। यह एक विशिष्ट प्रत्याभूति है जो केवल एक संव्यवहार के रूप में दी गई है। यह प्रत्याभूति जिस संव्यवहार के विषय में दी जाती है, उसके पूर्ण होते ही समाप्त हो जाती है।
(2) चलत प्रत्याभूति (Continuing Guarantee)- जो प्रत्याभूति संव्यवहारों की किसी श्रृंखला तक विस्तृत होती है, उसे निरन्तर प्रत्याभूति कहते हैं।
प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल – किसी अन्य संविदा की भाँति प्रत्याभूति की संविदा भी प्रतिफल द्वारा समर्थित होनी चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 127 के अनुसार, “मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिये जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा।”
अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभू के द्वारा प्रतिफल प्राप्त ही किया गया हो। प्रतिभू के द्वारा की गई प्रतिज्ञा मुख्य ऋणी व ऋणदाता के बीच मान्य प्रतिफल होती है, या मुख्य ऋण के लाभ के लिए जो भी कार्य किया गया हो, वह प्रतिभू की प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल है।
उदाहरण- दृष्टान्त (क) — ‘क’ से ‘ख’ माल उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। ‘क’ वैसा करने को इस शर्त पर रजामन्द हो जाता है कि ‘ग’ माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति दे। ‘क’ के इस वचन के प्रतिफलस्वरूप कि वह माल परिदान करेगा, ‘ग’ संदाय की प्रत्याभूति देता है। यह ‘ग’ के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।
दृष्टान्त (ख) –‘ख’ को ‘क’ माल बेचता है और परिदत्त करता है। ‘ग’ तत्पश्चात् प्रतिफल के बिना करार करता है कि ‘ख’ द्वारा व्यतिक्रम होने पर वह माल के लिए संदाय करेगा। करार शून्य है।
प्रसनजीत मेहता बनाम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ए० आई० आर० (1979) पटना 151 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया है कि “यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य ऋणी के लिए जो भी कुछ कार्य या प्रतिज्ञा की गई हो, वह प्रतिभू की इच्छा पर हो।” भूतकालीन ऋण के लिए दी गई प्रत्याभूति शून्य होगी।
जबकि मूल ऋणी का भूतकालीन लाभ प्रत्याभूति के बन्धनामा (Bond of Guarantee) के लिए समुचित प्रतिफल हो सकता है। इससे सम्बन्धित वाद गुलाब हुसैन बनाम फैय्याज अली खाँ, ए० आई० आर० (1940) अवध 346 में एक व्यक्ति ने पट्टे के बकाया किराये को किश्तों में चुकाने की प्रतिज्ञा किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी ने उस व्यक्ति की प्रत्याभूति दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह मान्य प्रतिभूति की संविदा है। अतः प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। राम नारायण बनाम हरी सिंह, ए० आई० आर० (1964) राज० 76 के वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि मूल ऋणी को भूतकाल में दिया गया फायदा अर्थात् प्रत्याभूति देने से पूर्व मूल ऋणी के लाभ के लिए किया गया कार्य प्रत्याभूति की संविदा के लिए पर्याप्त प्रतिफल नहीं होगा।
पंजाब नेशनल बैंक बनाम माया इण्टरप्राइजेज, ए० आई० आर० (2003) एन० ओ० सी० 299 (दिल्ली) के बाद में प्रतिवादी ने बादी के पक्ष में एक जवाबी प्रत्याभूति दिया कि यदि वादी को बैंक की प्रत्याभूति के अन्तर्गत भुगतान करना पड़ा तो वह जवाबी प्रत्याभूति से अपने आप को सुरक्षित कर लेगा अर्थात् जवाबी प्रत्याभूति के अन्तर्गत वादी प्रतिवादी के विरुद्ध भुगतान प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न 5. सतत् प्रत्याभूति से आप क्या समझते हैं? क्या सतत् प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण हो सकता है? What do you understand by Continuing Guarantee. Can a Continuing Guarantee be revoked?
उत्तर- सतत प्रत्याभूति (Continuing Guarantee) — संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 129 चलत या सतत प्रत्याभूति की परिभाषा देती है कि, “वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों को किसी आवली पर हो, चलत या सतत प्रत्याभूति” कहलाता है।
जैसे- ‘क’ एक चाय के व्यापारी ‘ख’ को, उसे चाय के लिए, जिसका वह ‘ग’ को समय-समय पर प्रदाय करे, 100 पौण्ड तक की रकम का संदाय करने की प्रत्याभूति देता है। ‘ग’ को ‘ख’ उपर्युक्त 100 पौण्ड से अधिक मूल्य की चाय का प्रदाय करता है और ‘ग’ ‘उसके लिए ‘ख’ को संदाय कर देता है। तत्पश्चात् ‘ग’ को ‘ख’ 200 पौण्ड मूल्य की चाय का प्रदाय करता है। ‘ग’ रकम संदाय करने में असफल रहता है। ‘क’ द्वारा दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति थी, और तदनुसार वह ‘ख’ के प्रति 100 पौण्ड तक ही दायी है।
अर्थात् जब प्रत्याभूति का विस्तार एक संव्यवहार तक सीमित न होकर कई संव्यवहार के कई भागों (आवली) पर विस्तारित रहता है तो उसे चलत प्रत्याभूति कहते हैं। जो प्रत्याभूति केवल एक संव्यवहार के लिए दी गई हो, वह उस संव्यवहार के पूरे होते ही समाप्त हो जाती. है परन्तु चलत प्रत्याभूति निश्चित समय तक चलती रहती है। के० बनाम ग्रोब्स, (1829) 80 इ० आर० 1274 के तथ्यों पर दृष्टान्त (ग) आधारित है जिसमें कि “इस प्रत्याभूति द्वारा कि मैं ‘क’ के प्रति आटे के पाँच बोरे जो वह ‘ख’ को बेचेगा और जिसका भुगतान एक माह में होना है, दायी होऊंगा, पाँच बोरे दिये गये और ‘ख’ ने उनके मूल्य का भुगतान कर दिया। उसी माह में और माल उसे दिया गया जिसका कि ‘ख’ ने भुगतान नहीं किया। प्रतिभू पर वाद लाया गया।
निर्णीत हुआ कि यह चलत प्रत्याभूति नहीं थी, अतः वाद में दिये जाने वाले माल के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं था।
साधारण प्रत्याभूति केवल एक संव्यवहार या निश्चित धन तक एक से अधिक संव्यवहारों के लिए होती है और उनका भुगतान होते ही समाप्त हो जाती है परन्तु चलत प्रत्याभूति चालू खाते के समान होती है जिसका बैलेन्स घटता-बढ़ता रहता है और जो अवधि समाप्त होने पर न चुकाये हुए ऋण के लिए प्रतिभू को दायी बनाती है।
किसी कर्मचारी को ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं होती क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति मात्र एक संव्यवहार है। जब तक कर्मचारी पद पर रहता है या प्रत्याभूति का समय समाप्त नहीं होता है तब तक प्रत्याभूति बनी रहती है। जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया है उसकी ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वाद दुर्गा प्रिया चौधरी बनाम दुर्गा पद राय, ए० आई० आर० (1928) कलकत्ता 204 के निर्णय के अनुसार, चलत प्रत्याभूति मानी गयी।
चलत प्रत्याभूति की स्थिति में प्रतिभू अपने दायित्व की सीमा निश्चित कर सकता है। जैसे- ‘वन्दना’ अपनी मित्र ‘माला’ को वचन देती है कि यदि वह ‘रीना’ को माल की आपूर्ति करती है तो एक वर्ष के अन्दर, वह जो भी माल ‘रीना’ को देगी उसके लिए ‘रीना’ द्वारा माल की कीमत न दिये जाने पर ‘वन्दना’ 5,000 रुपये तक उत्तरदायी होगी।
चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण (धारा 130) – संविदा अधिनियम की धारा 130 चलत प्रत्याभूति के प्रतिसंहरण के विषय में बतलाती है। इस धारा के अनुसार, “चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी समय भी प्रतिभू कर सकेगा।”
अतः चलत प्रत्याभूति के प्रतिसंहरण का प्रथम तरीका यह है कि प्रतिभू भविष्य के संव्यवहारों के लिए प्रतिसंहरण की सूचना देकर अपने द्वारा दी गई प्रत्याभूति को वापस ले सकता है। भविष्य में कोई ऋण या वस्तुओं को देने के लिए दी गई प्रत्याभूति तभी बाध्यकारी होगी जबकि उस व्यक्ति ने जिसको प्रत्याभूति दी गई है, उस पर कार्य किया हो। परन्तु उस पर कार्य किये जाने के पूर्व प्रत्याभूति वापस ली जा सकती है। कार्य किये जाने के बाद भी शेष संव्यवहारों के लिए प्रत्याभूति वापस ली जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक संव्यवहार स्वतन्त्र होता है।
‘दृष्टान्त (ख) –’ख’ को ‘क’ 1,000 रुपये तक की प्रत्याभूति देता है कि ‘ग’ उन सब विनिमय-पत्रों का, जो ‘ख’ उसके नाम लिखेगा, संदाय करेगा। ‘ग’ के नाम ‘ख’ विनिमय- पत्र लिखता है। ‘ग’ उस विनिमय पत्र को प्रतिग्रहीत करता है। ‘क’ प्रतिसंहरण की सूचना देता है। ‘ग’ उस विनिमय-पत्र को उसके परिपक्व होने पर अनादृत कर देता है। ‘ग’ अपनी प्रत्याभूति के अनुसार दायी है।
आफोर्ड बनाम डेविस के वाद में एक वर्ष के अन्तर्गत 600 पौण्ड की सीमा तक डेविस एण्ड कम्पनी जितने भी बिलों की कटौती पर भुगतान लेगी, प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। लेकिन भुगतान के पहले ही प्रत्याभूति वापस ले ली गई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी अपनी प्रत्याभूति वापस ले सकता है।
प्रश्न 6. प्रतिभू के दायित्व की विवेचना कीजिए। क्या प्रतिभू को अपने दायित्व की सीमा निर्धारण का अधिकार है? Discuss the nature of Surety’s Liability? Is surety has a right to determine limitation of his liability?
अथवा (Or)
क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी केसाथ सम-विस्तीर्ण है? Do you agree with the view that the liability of surety is coextensive with that of Principal debtor. Refer the decided cases.
उत्तर- क्या प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सम-विस्तीर्ण (Co-extensive) है?— प्रतिभू के दायित्व की सीमा क्या होगी, यह संविदा अधिनियम की धारा 128 में वर्णित है। धारा 128 के अनुसार, प्रतिभू का दायित्व उतना ही है जितना मूल ऋणी का। परन्तु संविदा के माध्यम से प्रतिभू अपना दायित्व सीमित कर सकता है अर्थात् किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के समान ही रहता है। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सम-विस्तीर्ण (Co-extensive) है, अर्थात् (1) प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के साथ-साथ चलता है; तथा (2) प्रतिभू उतना ही उत्तरदायी होगा जितना मूल ऋणी न उससे कम न उससे अधिक ।
धारा 128 सामान्य विधि के सिद्धान्त को स्थापित करती है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होता है “जब तक कि कोई प्रतिकूल संविदा न हो” का अर्थ बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अवरत भगवन्त नायक, ए० आई० आर० (2005) बाम्बे 224 के बाद में निर्धारित किया गया कि “यह दायित्व के विषय में उपर्युक्त नियम के अन्यथा कोई उपबन्ध” अभिप्रेत है। एम० सी० पोनप्पा बनाम स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ए० आई० आर० (2015) एन० ओ० सी० 330 कर्नाटक के बाद में बैंक द्वारा ऋण की वसूली के वाद में यह माना गया कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सम विस्तीर्ण होता है। प्रतिभू इस दायित्व से अपने को बचा नहीं सकता।
धारा 128 के उदाहरण के अनुसार, एक ऋण के भुगतान की प्रतिभूति के मामले में प्रतिभू केवल मूल ऋण के लिए ही नहीं अपितु उसके अन्तर्गत ब्याज तथा आवश्यक खर्ची के लिए भी उत्तरदायी होगा।
बैंक ऑफ बिहार बनाम डॉ० दामोदर प्रसाद, ए० आई० आर० 1969 सु० को० 297 के मामले में दामोदर प्रसाद ने एक बैंक द्वारा दिये गये ऋण के लिए प्रतिभूति दी। मूल ऋणी की चूक पर बैंक ने प्रतिभू पर वाद किया। दामोदर प्रसाद का यह तर्क था कि ऋण पहले मूल ऋणी से वसूल किया जाना चाहिए अर्थात् ऋण वसूली हेतु पहले मूल ऋणी पर बाद लाया जाना चाहिए तथा प्रतिभू के कारण उसका दायित्व मूल ऋणी के पश्चात् आता है।
उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी दामोदर प्रसाद के उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ-साथ बना रहता है तथा लेनदार के लिए यह विकल्प है कि वह ऋण वसूली हेतु बाद या तो मूल ऋणी के विरुद्ध लाये या प्रतिभू के विरुद्ध प्रतिभू लेनदार को यह नहीं कह सकता कि वह पहले मूल ऋणी पर कार्यवाही करे। न्यायालय के अनुसार प्रतिभू ऋण के भुगतान का आश्वासन देता है कि मूल ऋणी भुगतान करेगा इसलिए उसका कर्तव्य है कि ऋण का भुगतान करवाये। यदि लेनदार को मूल ऋणी से भुगतान की निश्चितता रहती तो वह प्रतिभू की आवश्यकता क्यों महसूस करता।
परन्तु बाद के एक वाद यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मंकू नारायण, ए० आई० आर० 1987 सु० को० 1078 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऋणदाता को पहले बन्धकवद्ध सम्पत्ति से ऋण वसूलने की कार्यवाही करनी चाहिए फिर शेष के लिए प्रतिभू के विरुद्ध ।
यह एक सुव्यवस्थित नियम है कि ऋणदाता प्रतिभू के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व मूल ऋणी के प्रति समस्त उपचार प्राप्त करने या वाद प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ तक कि ऋणदाता प्रतिभू के ही विरुद्ध कार्यवाही करे और मूल ऋणी को स्पर्श ही न करे या तो ऋणदाता एक ही साथ प्रतिभू व मूल ऋणी दोनों के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।
वसीकॉम लिमिटेड बनाम हरजिन्दर सिंह, ए० आई० आर० (2006) ए० सी० 1874 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऑफ बिहार बनाम डॉ० दामोदर प्रसाद के बाद में दिये गये सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि मूल ऋणी के चूक की अवस्था में प्रतिभू का दायित्व तुरन्त उत्पन्न होता है, प्रतिभू यह तर्क देकर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता कि लेनदार मूल ऋणी के विरुद्ध समस्त उपचार समाप्त कर ले, तत्पश्चात् उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।
सिण्डीकेट बैंक बनाम के० मनोहरा, ए० आई० आर० (2003) केरल 284 के मामले में न्यायालय द्वारा प्रतिभू तथा मूल ऋणी को संयुक्ततः तथा व्यक्तितः दायी ठहराया गया।
प्रतिभू भी ऋणी की स्थिति में होता है, यदि ऋणदाता कोई प्रतिभूति माँगे तो प्रतिभू भी अन्य ऋणियों की भाँति अपनी सम्पत्ति को सम्यक् बन्धक के अधीन डाल सकता है।
राम किशन एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० एण्ड अदर्स, ए० आई० आर० (2012) सु० को० 2288 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि धारा 128- प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होता है तो उसे अपने विरुद्ध यह तर्क देकर डिक्री के निष्पादन को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध समस्त उपचार का प्रयोग नहीं कर ले।
दायित्व की सीमा – प्रत्येक प्रतिभू को अपने दायित्व की सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। वह अपनी प्रत्याभूति में यह कह सकता है कि, “मेरा दायित्व 500 रुपये तक सीमित होगा।” ऐसी परिस्थिति में मूल ऋणी का दायित्व कुछ भी हो, प्रतिभू का दायित्व, इस प्रकार से निर्धारित की गई सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता।
प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के सम-विस्तीर्ण होता है। यह उक्ति दायित्व की सीमा निर्धारित करती है जब तक कि इसे प्रतिबन्धित न किया जाय। यदि मौलिक संविदा शून्य है, जैसे अवयस्क की संविदा तो प्रतिभू मूल ऋणी के समान उत्तरदायी होगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम सी० एल० विमला, ए० आई० आर० (2015) एस० सी० 2280 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणो के दापित्व के समविस्तीर्ण होता है। प्रत्याभूति खण्ड में प्रतिभू ऋणदाता के द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध – किसी भी निर्णय के प्रति सहमत था इसलिए बैंक व ऋणी के मध्य कोई समझौता, प्रतिभू पर बाध्यकारी था। टिक्की लाल बनाम कोमल चन्द, आई० एल० आर० (1940) नागपुर के वाद में न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि जब प्रतिभू ऋणदाता से ऋणी का प्रतिनिधित्व करता है कि वह संविदा के योग्य है और यदि निरूपण असत्य साबित होता है तो स्वयं प्रतिभू उत्तरदायी होगा, अर्थात् प्रतिभू प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा। विधि के प्रवर्तन द्वारा मूल ऋणी की उन्मुक्ति प्रतिभू की उन्मुक्ति पर प्रभाव नहीं डालती। इससे सम्बन्धित मोहम्मद बनाम अब्दुल, (1939) लाहौर 187 के बाद में दो विरोधी पक्षकारों का विवाद पंचनिर्णय को सौंपा गया। एक व्यक्ति (प्रतिभू) ने एक पक्षकार के लिए पंचनिर्णय द्वारा प्रदत्त राशि को देने के लिए प्रत्याभूति दिया। प्रतिभू ने निर्णीत राशि का भुगतान कर दिया तथा मूल ऋणी के विरुद्ध जमा राशि की प्राप्ति के लिए वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रतिभू को उक्त राशि पाने का अधिकारी बताया। यद्यपि पंचनिर्णय को सौंपा गया विवाद शून्य एवं अवैध था यदि मूल ऋणी दिवालिया घोषित हो जाय तो वह स्वयं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, परन्तु प्रतिभू को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। उसे अपने दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती।
सी० पी० लाल बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तिरुवनन्थपुरम् तथा अन्य, ए० आई० आर० 2007 केरल 131 के बाद में प्रत्याभूति को संविदा में कोई वाक्यांश देनदार को अधिकृत करता है कि वह इस प्रकार कार्य करने की स्थिति में प्रत्याभूति तब तक लागू रहेगी, जब तक ऋणदाता पूरे ऋण का भुगतान नहीं करता है। परिसीमा उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रतिभू माँग या ऋण का भुगतान करने से इन्कार कर देता है।
प्रश्न 7. (i) प्रतिभू के अधिकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। Discuss the rights of surety in detail.
(ii) सह-प्रतिभू के दायित्वों की विवेचना कीजिए। Discuss the liability of co-surety.
उत्तर (i) – वह व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है, प्रतिभू कहलाता है। प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू के निम्न व्यक्तियों के प्रति अधिकार निम्न प्रकार से हैं-
(1) मूल ऋणी के विरुद्ध प्रत्यासन का अधिकार (धारा 140 )
(2) मूल ऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार (धारा 145)
(3) लेनदार के विरुद्ध प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार (धारा 141)
(4) सह प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार (धारा 146-147)
(1) प्रत्यासन का अधिकार- ऐसे सभी अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के प्रति प्राप्त थे, प्रतिभू में समाहित हो जाते हैं बशर्ते कि (i) प्रत्याभूत ॠण शोध्य हो गया हो तथा मूल ऋणी प्रत्याभूत कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया हो; या (ii) प्रतिभू ने दायित्वाधीन ऋण का भुगतान कर दिया हो। अन्तरण के बिना, विधि या साम्या उन समस्त अधिकारों को प्रतिभू में समाहित कर देती है। इसे प्रत्यासन का अधिकार कहते हैं प्रतिभू को यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जब कि वह लेनदार के प्रति अपना सम्पूर्ण दायित्व पूर्ण कर लेता है। यह कहा जाता है कि प्रतिभू ऋण का भुगतान करने के पश्चात् लेनदार का स्थान ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए रि लैम्पले आइस ओर कम्पनी लि० (1927) 1 चान्सरी डिवीजन 308 के बाद में एक निदेशक ने कम्पनी के द्वारा किराया दिये जाने की प्रतिभूति दी थी। इसी बीच कम्पनी का परिसमापन प्रारम्भ हो गया। प्रतिभू को किराये का भुगतान अदा करना पड़ा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मकान मालिक को जो अधिकार कम्पनी के प्रति प्राप्त थे, वे अधिकार किराये का भुगतान करने के बाद प्रतिभू को प्राप्त होंगे।
यदि पूर्वदेय धनराशि से धनराशि देकर प्रतिभू दायित्व से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह मूल ऋणी से केवल उतनी ही धनराशि वसूल कर सकता है जितना कि वास्तव में उसने दिया है।।
(2) क्षतिपूर्ति का अधिकार (थारा 145) क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 145 में प्रावधान किया गया है। धारा 145 के अनुसार प्रतिभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किये जाने का मूल ऋणी का विवक्षित वचन रहता है और प्रतिभू किसी भी धनराशि को जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकारपूर्वक दी हो, मूल ऋणी से वसूल करने का अधिकारी है। परन्तु उन धनराशियों की वसूली नहीं कर सकेगा जो उसने अनधिकारपूर्वक दी हो।
(क) ‘ग’ का ‘ख’ ऋणी है और ‘क’ उस, ऋण के लिए प्रतिभू है। ‘ग’ संदाय की माँग ‘क’ से करता है और उसके इनकार करने पर उस रकम के लिए उस पर वाद लाता है। प्रतिरक्षा के लिए युक्तियुक्त आधार होने से ‘क’ बाद में प्रतिरक्षा करता है, किन्तु वह ऋणी की रकम को खर्च समेत संदत्त करने के लिए विवश किया जाता है। वह मूल ऋण तथा अपने द्वारा दी गयी खर्चे की रकम को भी वसूल कर सकता है।
(ख) ‘ग’ द्वारा ‘ख’ को प्रदाय किये जाने वाले चावल के लिए ‘क’ 2,000 रुपये तक का संदाय प्रत्याभूत करता है। ‘ख’ को ‘ग’ 2,000 रुपये से कम की रकम का चावल प्रदाय करता है, किन्तु प्रदाय किये गये चावल के लिए ‘क’ से 2,000 रुपये की राशि का संदाय अभिप्राप्त कर लेता है। ‘क’ वास्तव में प्रदाय किये गये चावल की कीमत से अधिक ‘ख’ से वसूल नहीं कर सकता है।
इसके अलावा प्रत्याभूति की संविदा के अन्तर्गत प्रतिभू ने जो भी धनराशि वैध रूपेण लेनदार को भुगतान किया हो वह उस धनराशि को मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है क्योंकि संविदा में यह उपलक्षित प्रतिज्ञा होती है कि मूल ऋणी उस लिये हुए ऋण की क्षतिपूर्ति करेगा। प्रतिभू केवल सही रूप से दिये गये धन को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि प्रतिभू को कम धन की अदायगी करने के बाद ही छुटकारा मिल जाता है तो वह पूरा ऋण वसूल नहीं कर सकता है। अवैध रूप से दिये गये धन पर क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है।
(3) प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने का अधिकार- इस अधिनियम की धारा 141 में प्रतिभू के प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रतिभू प्रत्येक ऐसी प्रतिभूति के लाभ पाने का अधिकार रखता है जो उस समय जब प्रत्याभूति की संविदा की जाए लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो; चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मुख्य परिणाम तक उन्मोचित हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप-
(क) ‘क’ की प्रत्याभूति पर ‘ग’ अपने अभिधारी ‘ख’ को 2,000 रुपये उधार देता है। ‘ग’ के पास उन 2,000 रुपयों के लिए ‘ख’ के फर्नीचर के बन्धक के रूप में एक और प्रतिभूति है। ‘ग’ उस बन्धक को रद्द कर देता है। ‘ख’ दिवालिया हो जाता है और ‘ख’ की प्रत्याभूति के आधार पर ‘क’ के विरुद्ध ‘ग’ वाद लाता है। ‘क’ उस फर्नीचर के मूल्य की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया है।
कभी-कभी प्रतिभूति की संविदा में मूल ऋणी प्रतिभूति रखता है तो जो भी प्रतिभूतियाँ लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हैं उन्हें प्रतिभू ऋण का भुगतान करने के बाद प्राप्त करने के बाद करने का अधिकारी होता है चाहे उसे उसका ज्ञान हो या नहीं प्रतिभूति संविदा के पश्चात् ही क्यों न दी गयी हो। यदि लेनदार उन प्रतिभूतियों को खो देता है तो प्रतिभू की सहमति के बिना त्याग देता है तो प्रतिभू उनके मूल्यों की सीमा तक उन्मुक्त हो जायेगा। फोर्बोस बनाम जैम्सन, (1872) 19 चा० डि० 615 के वाद में एक व्यक्ति ने पट्टे की सम्पत्ति व बीमा पॉलिसी को बन्धक रखकर 200 पौण्ड ऋण लिया। प्रतिवादी प्रतिभू हुआ। उसके ज्ञान के बिना मूल ऋणी ने उन्हीं प्रतिभूतियों पर अधिक ऋण लिया। मूल ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर प्रतिभू ने व्याज़ का भुगतान करके दोनों प्रतिभूतियाँ वापस माँगी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरे ऋण से प्रतिभू का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। यदि दी गयी प्रतिभूति उस स्थिति में न हो तब भी प्रतिभू उन्मुक्त हो जायेगा। ये नियम तभी लागू होंगे जब प्रतिभू ने ऋण का भुगतान कर दिया हो अर्थात् प्रतिभू प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने योग्य तभी होता है जब उसने अपना दायित्व चुका दिया हो। इब्राहिम अब्दुल लतीफ शेख बनाम कारपोरेशन बैंक, ए० आई० आर० (2003) कर्नाटक, 98 के वाद में निर्णीत किया गया है कि ऐसे प्रभाव रखने वाले करार की अनुपस्थिति में, प्रतिभू ऋणदाता से यह नहीं कह सकता कि वह एक समय विशेष पर प्रतिभूतियों से ऋण वसूलेगा। उसके द्वारा प्रतिभूतियों की वसूली न करने से प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता।
(4) सहप्रतिभू के विरुद्ध अंशदान प्राप्त करने का अधिकार- जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू हों तो उन्हें सहप्रतिभू कहते हैं। कभी-कभी लेनदार उस सह प्रतिभू में से किसी को सहप्रतिभू के दायित्व से उन्मोचित कर सकता है इससे दूसरे प्रतिभू के दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिस प्रतिभू को इस प्रकार दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, वह अन्य सह प्रतिभुओं को अपने अंश का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
जहाँ कि सह प्रतिभू हो वहाँ लेनदार दया द्वारा उनसे एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है।
जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही ऋण के लिए प्रतिभू का स्थान ग्रहण करते हैं तो मूल ऋणी द्वारा भुगतान न करने पर प्रत्येक सहप्रतिभू बराबर अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे ‘क’ ने ‘ख’ से 1,200 रुपये ऋण लिया जिसके लिए ‘ग’, ‘घ’, ‘च’ ने प्रतिभूति दी। ‘क’ ने ऋण अदायगी नहीं किया। ‘ग’, ‘घ’, ‘च’ बराबर अंशदान करके लेनदार को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।
निम्न दशाओं में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होती- (i) प्रतिभू का दायित्व भिन्न ऋणों के लिए हो;
(ii) संविदा के अन्तर्गत अंशदान न करने का निश्चय हुआ हो;
(iii) सह-प्रतिभू ने मिथ्या व्यपदेशन में कोई संविदा किया हो।
इस प्रकार जब लेनदार किसी सह प्रतिभू को दायित्व से मुक्त कर देता है तो इस कारण दूसरे सह-प्रतिभू को दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती तथा लेनदार द्वारा मुक्त किया गया सह-प्रतिभू, अन्य सह-प्रतिभू के प्रति दायित्व से मुक्त नहीं होता।
उत्तर (ii) – सह-प्रतिभू के दायित्व – जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू हों तो उन्हें सह-प्रतिभू कहते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 138 के अनुसार, “जहाँ कि सह-प्रतिभू हों वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है।”
श्री चन्द बनाम जगदीश प्रसाद किशन चन्द, (1966) 3 एस० सी० आर० के बाद में कहा गया कि लेनदार अपनी इच्छानुसार किसी भी सह-प्रतिभू को दायित्व से मुक्त कर सकता है। इससे दूसरे प्रतिभू के दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु जिस सह- प्रतिभू को इस प्रकार दायित्व मुक्त कर दिया जाता है, वह अन्य सह-प्रतिभू के प्रति अपना अंश भुगतान करने के लिए दायी रहता है।
जब एक हो ऋण के लिए एक से अधिक प्रतिभू बने हों और मूल ऋणों में त्रुटि की हो तो प्रत्येक सह-प्रतिभू को मूल ऋण का भुगतान करने के लिए बराबर-बराबर अभिदान करना होगा। जैसे कि, तीन सह-प्रतिभू हैं और मुख्य ऋणी 3,000 रुपये देने में असफल रहा है तो प्रत्येक सह-प्रतिभू का दायित्व बराबर-बराबर होगा चाहे सामूहिक हो या व्यक्तिगत, चाहे वे भिन्न-भिन्न धन के लिए प्रतिभू हों, चाहे उन्हें यह न मालूम हो कि और भी सह-प्रतिभू हैं।
सह-प्रतिभू जो विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध हैं, अपनी-अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओं तक सामान्यतः संदाय करने के दायी हैं। (धारा 147)
कमाल चन्द बनाम सुशीला वाला, (1938) कलकत्ता 405 के वाद में अभिनिर्णीत किया गया कि ‘कभी-कभी प्रतिभू के दायित्व की सीमा भिन्न-भिन्न होती है तो ऐसी स्थिति में सह-प्रतिभू उत्तरदायित्व की सीमा तक अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे’। अर्थात् जब एक प्रतिभू अपने अंश से ज्यादा दे देता है तो अन्य सह-प्रतिभू के विरुद्ध अंशदान करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, जैसे-
धारा 147 का दृष्टान्त (क) ‘घ’ के प्रतिभुओं के रूप में ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ इस शर्त पर आश्रित हैं कि ‘ङ’ को ‘घ’ सम्यक् रूप से लेखा देगा, पृथक् पृथक् तीन बन्ध-पत्र लिख देते हैं जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात् ‘क’ का 10,000 रुपये की, ‘ख’ का 20,000 रुपये की, ‘ग’ का 40,000 रुपये की शास्ति वाला है। ‘ग’ 30,000 रुपये का लेखा नहीं देता। ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ हर एक 10,000 रुपये संदाय करने के दायी हैं।
प्रश्न 8 प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन किस प्रकार होता है? How does the liability of surety discharges?
उत्तर – एक प्रतिभू अपने दायित्व से निम्न परिस्थितियों में उन्मुक्त होता है-
(1) निरसन की सूचना द्वारा प्रतिसंहरण करने से
(2) प्रतिभू की मृत्यु द्वारा
(3) संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा
(4) मूल ऋणी के उन्मोचन द्वारा
(5) ऋणदाता के समय, प्रशमन, दावा न करने के द्वारा
(6) प्रतिभू को क्षति पहुँचाने वाले कार्य या अकार्य द्वारा
(7) ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति को खो देने से
(8) मूल ऋणी द्वारा मिथ्या वर्णन करने से
(9) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रतिभू के साथ शामिल न होने से।
(1) सूचना द्वारा प्रतिसंहरण- चल प्रत्याभूति को प्रतिभू, लेनदार को सूचना देकर भविष्य के संव्यवहारों को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिसंहरण की सूचना के पूर्व के संव्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिभू का दायित्व बना रहता है परन्तु सूचना के पश्चात् लेनदार व मूल ऋणी के मध्य होने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ ‘ख’ को ‘क’ 1,000 रुपये तक की प्रत्याभूति देता है कि ‘ग’ उन सब विनिमयपत्रों का जो ‘ख’ उसके नाम लिखेगा संदाय करेगा। ‘ग’ के नाम ‘ख’ विनिमय पत्र लिखता है। ‘ग’ उस विनिमय पत्र को प्रतिग्रहीत करता है। ‘क’ प्रतिसंहरण को सूचना देता है। ‘ग’ उस विनिमयपत्र को उसके परिपक्व होने पर अनादूत कर देता है। ‘ग’ अपनी प्रत्याभूति के अनुसार दायी है।
आफोर्ड बनाम डेविस, 133 आर० आर० 491 के बाद में एक वर्ष के अन्तर्गत 600 पौण्ड की सीमा तक डेविस एण्ड कम्पनी जितने भी बिलों की कटौती पर भुगतान लेगी, प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। लेकिन भुगतान से पहले ही प्रत्याभूति वापस ले ली गई है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी अपनी प्रत्याभूति वापस ले सकता है।
(2) मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण- इसकी व्याख्या धारा 131 में की गयी है। प्रतिभू की मृत्यु पर चलत प्रत्याभूति का भविष्य के संव्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिसंहरण हो जाता है जब तक कि इसके विपरीत कोई संविदा न हो। प्रतिभू की मृत्यु की स्थति में, मृत्यु के पूर्व हुए संव्यवहारों के लिए प्रतिभू की सम्पदा दायी होती है परन्तु मृत्यु के बाद संव्यवहारों के लिए उसकी सम्पदा दायी नहीं होगी।
आंग्ल विधि के अन्तर्गत प्रतिभू की मृत्यु पर मृत्यु के पश्चात् संव्यवहारों के लिए प्रतिभू की सम्पदा तब दायी नहीं होगी जबकि लेनदार को प्रतिभू के मृत्यु की सूचना हो।
(3) संविदा की शर्तों में परिवर्तन द्वारा प्रतिभू का उन्मोचन – विधि का सामान्य नियम है कि प्रतिभू संविदा के अन्य पक्षकारों की भाँति उस कार्य के लिए बाध्य नहीं होगा जिसके लिए उसने संविदा की ही नहीं है। प्रतिभू के हितों की रक्षा ही साम्या या विधि का लक्ष्य है अतः इसका उत्तरदायित्व विधि के नियमानुसार नियमित होता है। यदि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रतिभू की सम्मति के बिना संविदा में कोई सारभूत परिवर्तन कर देता है तो उसके पश्चात् होने वाले संव्यवहारों के लिए प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होता अर्थात् प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। नये पदों के पुनः स्थापन से मौलिक संविदा की स्थिति भिन्न होती है जिसके लिए उसने सम्मति दी ही नहीं तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होगी।
बोनोर बनाम मैक्डोनाल्ड, (1850) 3, एच० एल० सी० 226 के वाद में प्रतिवादी ने एक बैंक मैनेजर के आचरण की प्रत्याभूति दिया। उसकी सहमति के बिना बैंक मैनेजर के वेतन में वृद्धि इस आधार पर की गई कि वह स्वयं के द्वारा किये गये बट्टे पर होने वाली हानि के 1/4 भाग के लिए उत्तरदायी होगा। एक बट्टे में हानि हुई। न्यायालय ने प्रतिभू को दायित्वों से मुक्त किया; क्योंकि जिस संविदा में उसने प्रतिभू दी थी उसमें उसकी सहमति के बिना परिवर्तन किया गया। यदि संविदा के पदों में परिवर्तन पक्षकारों के कार्य द्वारा न होकर विधि के द्वारा होता है तब भी प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है।
सतीश चन्द्र जैन बनाम नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, ए० आई० आर० (2003) सु० को० 623 के वाद में पुत्र के व्यक्तिगत कारोबारी ऋणों के लिए प्रत्याभूत कारोबार संगठन को कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। पुत्र व उसका एक सहयोगी उन्हों ऋणों के लिए दो नये प्रतिभू बन गये। उसके पिता जो प्रतिभू थे उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सकी।
विश्वनाथ अग्रवाल बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० (2005) झारखण्ड 69 के वाद में एक बैंक गारण्टी जिसमें प्रतिभू ने 2,50,000 रुपये की सीमा तक प्रत्याभूति दिया था, परन्तु बैंक ने उक्त धन की सीमा से अधिक ऋण दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिभू उक्त धन की सीमा से अधिक धन के लिए दायी नहीं होगा।
सिक्किम उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम विवेक गर्ग, ए० आई० आर० (2011) सिक्किम 7 के मामले में निर्णय दिया कि “गारण्टी करार में यह कह दिया गया था कि किसी प्रकार के समझौते द्वारा गारण्टी के निबन्धनों में किसी भी फेरफार से प्रतिभू दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा। इसके बारे में यह माना जायेगा कि उसने पहले से अपनी सहमति दे रखी है। वह अपने दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम वीराधुरगर स्टील रोलिंग मिल्स लि०, ए० आई०आर० (2016) ए० सी० 191 के वाद में भी निदेशक अपने दायित्व से मुक्ति न पा सका। इसमें क्रान्ट्राप्रोफेरन्टम (Contraproferentum) रूल लागू किया।
(4) मूल ऋणी के उन्मोचन द्वारा लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाये या किसी ऐसे कार्य या लोप से जिसका विधिक परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन हो, तो प्रतिभू भी उन्मोचित हो जाता है। उदाहरण के लिए ‘ग’ द्वारा ‘ख’ को प्रदान किये जाने वाले माल के लिए ‘ग’ को ‘क’ प्रत्याभूति देता है। ‘ख’ को ‘ग’ माल प्रदाय करता है और तत्पश्चात् ‘ख’ संकट में पड़ जाता है और अपने लेनदारों से उनकी माँगों से अपने को निर्मुक्त किये जाने के प्रतिफल स्वरूप उनकी अपनी सम्मति समनुदेशित करने की संविदा करता है। यहाँ ‘ग’ के साथ की गयी इस संविदा द्वारा ‘ख’ अपने ऋण से निर्मुक्त हो जाता है और ‘क’ अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित हो जाता है।
इससे सम्बन्धित वाद कामर्शियल बैंक ऑफ तस्मानियां बनाम जोन्स, (1893) ए० सी० 313, 311 के वाद में लेनदार किसी नये ऋणी को पुराने ऋणी के स्थान पर स्वीकार कर लेता है तो पुराने ऋणी को दी गयी प्रत्याभूति समाप्त हो जाती है और प्रतिभू उन्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मूल ऋणी को किसी भी प्रकार से दी गयी छूट प्रतिभू पर भी लागू हो जाती है।
मेसर्स कुरनूल चीफ फण्ड्स प्रा० लिमिटेड बनाम पी० नरसिम्हा एवं अन्य, ए० आई० आर० (2008) आन्ध्र प्रदेश 38 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि मूल ऋणी के विरुद्ध दायर वाद यदि चूक के कारण खारिज कर दिया गया तथा अन्तिम रूप से निर्णीत हो गया तो प्रतिभू के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।
(5) लेनदारों द्वारा मूल ऋणी से समझौता करने पर – इसका प्रावधान धारा 135 में किया गया है-लेनदार और मूलऋणी के बीच ऐसी संविदा जिससे लेनदार मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेता है ‘या उसे समय देने या उस पर वाद न लाने का वचन देता है, प्रतिभू को तब के सिवाय उन्मोचित कर देती है जबकि प्रतिभू ऐसी संविदा के विरुद्ध अनुमति दे देता है।
(6) लेनदार के असंगत कार्य या कार्यलोप से यदि लेपदार कोई ऐसा कार्य को जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य की करने का लोप करे जिसके किये जाने को प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और मूलऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने पारिणामिक उपचार का तद्द्वारा हास हो तो प्रतिभू उन्मोचित हो जायेगा।
उदाहरण स्वरूप, ‘ख’ के फर्नीचर के ऐसे विक्रयाधिकार पत्र के साथ जो ‘ग’ को यह शक्ति देता है कि वह फर्नीचर बेच दे और उसके आगमों को वचन पत्र के उन्मोचन में उपार्जित कर लें। ‘ग’ के पक्ष में ‘ख’ द्वारा और ‘ख’ के प्रतिभू के रूप में ‘क’ द्वारा लिखे गये संयुक्त एवं पृथक् वचनपत्र की प्रतिभूति पर ‘ख’ को ‘ग’ धन उधार देता है। तत्पश्चात् ‘ग’ उस फर्नीचर को बेच देता है किन्तु उस उपचार से उसके द्वारा जानबूझकर की गयी उपेक्षा के कारण केवल थोड़ी कीमत प्राप्त होती है। ‘क’ उस वचन पत्र के दायित्व से उन्मोचित हो जाता है।
एम० आर० चक्रपाणी आयंगर बनाम केनरा बैंक, ए० आई० आर० 1997 फर्म 216 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि गिरवी रखी गयी सम्पत्ति मूल ऋणी द्वारा विक्रय की जाती है और प्रतिभू उसकी सूचना ऋणदाता को दे देता है। ऋणदाता उस सम्पत्ति को जब्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता या आपराधिक न्यायालय से मूल ऋणी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता तो प्रतिभू दायित्व से उन्मोचित हो जायेगा।
(7) लेनदार द्वारा प्रतिभूति खो देने से लेनदार जो ऋण देता है तथा ऋणी से प्रतिभूति प्राप्त करता है साथ ही उत्तरदायी होने की प्रतिज्ञा करता है मूल ऋणी द्वारा प्रतिज्ञा पालन न करने पर लेनदार प्रतिभू से उसकी प्रतिज्ञा का पालन करवा सकते हैं। यदि मूल ऋणी चूक करता है तो लेनदार मूल ऋणी से प्रतिभू या दोनों के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। लेनदार का यह कर्तव्य है कि प्रत्याभूति संविदा के अन्तर्गत जो भी प्रतिभूतियाँ दी गयी है उन्हें सुरक्षित रखे क्योंकि मूल ऋण प्राप्त होने पर उसका कर्तव्य है कि वह प्रतिभूतियों को मूल ऋणी को वापस करे। यदि वह व्यतिक्रम करेगा तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है।
(8) मूल ऋणी द्वारा मिथ्या वर्णन करना- धारा 142-143 के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिभूति प्राप्त करता है उसका कर्तव्य है कि वह तथ्य पूर्ण स्पष्टीकरण दे जिसका कि दायित्व पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अभाव में संविदा शून्यकरणीय मानी जायेगी। इस प्रकार प्रत्याभूति की संविदा को अमान्य होने के लिए आवश्यक है कि-
(1) यह मिध्या वर्णन द्वारा प्राप्त की गई हो;
(2) मिथ्या वर्णन लेनदार द्वारा किया गया हो जो संव्यवहार के सारभूत भाग के विषय में है।
(9) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिभू के साथ सम्मिलित न होने से प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है।
उपनिधान (Bailment)
(धाराएँ 148-171 एवं 180-181)
प्रश्न 9. उपनिधान (निक्षेपण) की परिभाषा दीजिए तथा उपनिधान के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।Define Bailment and briefly state the basic elements of Bailment.
उत्तर- उपनिधान (Bailment) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148 निक्षेप या उपनिधान की परिभाषा देती है। जब एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए अपनी किसी वस्तु को इस संविदा (शर्त) के साथ देता है कि दूसरा व्यक्ति उस प्रयोजन को पूर्ण होने के पश्चात् वस्तु (माल) का परिदान करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा निर्देशित किसी दूसरे व्यक्ति को वापस दे देगा तो ऐसी संविदा को उपनिधान की संविदा कहते हैं।
कपड़े दर्जी को सीने के लिए देना, कपड़े ड्राइक्लिनिंग के लिए ड्राइक्लीनर को देना, साइकिल या घड़ी मरम्मत हेतु देना, आभूषण निर्माण हेतु सोना या चाँदी देना उपनिधान संविदा के कुछ उदाहरण हैं।
जो व्यक्ति माल या वस्तु को किसी उद्देश्य के लिए परिदत्त करता है उसे उपनिधाता या निक्षेपक (Bailor) कहते हैं तथा जिस व्यक्ति को वस्तु या माल का परिदान किया जाता है वह उपनिहिती या निक्षेपग्रहीता कहलाता है।
इस प्रकार उपनिधान की संविदा तक ऐसे सम्बन्ध को जन्म देती है जिसमें एक चल (जंगम) सम्पत्ति कुछ निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति के कब्जे में चली जाती है। इस दौरान वस्तु या माल का स्वामित्व उपनिधाता के पास रहता है परन्तु कब्जा दूसरे व्यक्ति उपनिहिती (निक्षेपग्रहीता) के पास चला जाता है।
धारा 148 से जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि एक वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में रहती है तथा कब्जाधारी वस्तु के स्वामी से उक्त वस्तु को उपनिहिती के रूप में धारण करने की संविदा करता है तो उस संविदा के पश्चात् कब्जाधारी उपनिहिती हो जाता है तथा वस्तु का स्वामी उपनिधाता हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी कार ‘क’ को बेचता है परन्तु कार का कब्जा 6 माह के लिए अपने पास ही रखता है। उसका यह कब्जा उपनिहिती के रूप में होगा।
एक वैध उपनिधान के निम्न आवश्यक तत्व हैं –
(1) वस्तु या माल के कब्जे का एक व्यक्ति (वस्तु के स्वामी) से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण – उपनिधान का सबसे आवश्यक तत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु के कब्जे का अन्तरण है। इस प्रकार उपनिधान सिर्फ चल (जंगम) सम्पत्ति का हो सकता है। उपनिधान में वस्तु का स्वामित्व वस्तु के स्वामी (उपनिधाता) के पास बना रहता है। कब्जे का अन्तरण (परिदान) वास्तविक (Actual) तथा विवक्षित (Constructive) दोनों प्रकार से हो सकता है।
जब वस्तु का भौतिक कब्जा वास्तविक रूप से उपनिधाता से उपनिहिती को होता है अर्थात् जब वस्तु एक व्यक्ति के नियन्त्रण से दूसरे व्यक्ति के नियन्त्रण में वास्तव में प्रदत्त होती है तो यह वास्तविक अन्तरण (परिदान) कहा जाता है। परन्तु जब वस्तुतः वस्तु (माल) का कच्या उपनिहिती को न देकर कोई ऐसा कार्य किया जाय जिससे वस्तु पर कब्जा लेने का अधिकार उपनिहिती को प्राप्त हो जाय तो कब्जे के इस अन्तरण (परिदान) को विवक्षित या प्रलक्षित कब्जे का अन्तरण कहते हैं। (धारा 149) जैसे माल की बिल्टी देना या रेलवे रसीद देना। यहाँ माल एक व्यक्ति के पास बुक होता है तथा माल रेलवे को गोदाम में पड़ा होता है। परन्तु यदि प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिल्टी या रेलवे रसीद दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो माल पर नियन्त्रण रेलवे रसीद प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ही हो जायेगा।
जैसे ‘क’ एक सन्दूक जिसमें कुछ पुराने आभूषण रखे हैं सन्दूक सुनार को प्रदत्त कर यह निर्देश देता है कि सन्दूक में रखे आभूषण को गलाकर नये आभूषण बनाये। परन्तु सन्दूक की कुन्जी अपने पास रखता है। सन्दूक से पुराने आभूषण गायब हो जाते हैं। सुनार उत्तरदायी नहीं होगा क्योंक सन्दूक का वास्तविक कब्जा ‘क’ के पास है।
बैंक का लॉकर किराये पर लेना, उसमें वस्तुएँ रखना उपनिधान गठित नहीं करता। अतुल मेहरा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ए० आई० आर० (2003) पंजाब के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि उपनिधान गठित करने हेतु यह जरूरी है कि बस्तुएँ बैंक को दे दी जायें क्योंकि इसके बिना बैंक यह नहीं जान सकता कि उसमें क्या था और कितने मूल्य का था। बैंक व ग्राहक का सम्बन्ध मकान मालिक व किरायेदार के समतुल्य भी नहीं था क्योंकि ग्राहक स्वयं ही लॉकर तक पहुँचकर खोल नहीं सकता था, वह केवल बैंक को सहायता से ही ऐसा कर सकता था। लॉकर की लूट के समय भी इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वादी ने उसमें कुछ गहने आदि रखे थे।
(2) वस्तु का परिदान इस शर्त के साथ होना आवश्यक है कि वस्तु उस प्रयोजन के पूरा होने के पश्चात् उपनिधाता (स्वामी) या उपनिधाता द्वारा निर्देशित किसी व्यक्ति को लौटा दी जायेगी- यही आवश्यक तत्व उपनिधान की संविदा को विक्रय तथा दान की संविदा से पृथक् करता है। विक्रय तथा दान को संविदा में वस्तु का स्थायी परिदान (अन्तरण) होता है परन्तु उपनिधान में वस्तु का अन्तरण या परिदान अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस शर्त पर होता है कि प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर वस्तु (स्वामी) उपनिधाता को लौटा दी जाय।
उपनिधान की संविदा में वस्तु या तो उसी रूप में स्वामी को लौटायी जाती है या यदि वस्तु के परिवर्तन के उद्देश्य से वस्तु का अन्तरण हुआ है तो जाती है। जैसे दर्जी कपड़े को तथा सुनार सोने का परिवर्तित रूप वस्तु परिवर्तित रूप में लौटायी में वापस करता है। है। उदाहरण के रूप में बैंक में रुपया जमा करना उपनिधान नहीं है क्योंकि यहाँ बैंक वही नोट नहीं लौटाता जो जमा की गई होती है।
इस विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उपनिधान के लिए वस्तु या माल के कब्जे का अन्तरण किसी संविदा के अन्तर्गत होना आवश्यक है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद, ए० आई० आर० 1967 सु० को० 1885 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा के अभाव में भी उपनिधान का निर्माण होता है। इस वाद में वादी की दो ट्रक सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्त की। मुकदमें के दौरान ट्रकें बेच दी गईं। न्यायालय ने वादी को दोषमुक्त कर ट्रकें वापस करने का निर्देश दिया। न्यायालय के अनुसार ट्रकें जब्त करने के पश्चात् सरकार का ट्रकों पर कब्जा उपनिहिती के रूप में था तथा उसके लिए किसी संविदा की आवश्यकता नहीं थी। अतः सरकार ट्रकों के मूल्य के रूप में प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी थी। इसी प्रकार यदि चोरी का आभूषण पुलिस के कब्जे में है तो वह कब्जा उपनिहिती के कब्जे की भाँति है तथा यदि आभूषण चोरी हो जाते हैं तो सरकार उत्तरदायी होगी। वासवा के० डी० पाटिल बनाम मैसूर राज्य, ए० आई० आर० 1977, सु० को० 1749.
उपनिधान की संविदा यदि है तो वह लिखित या अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है। यह विवक्षित भी हो सकती है जैसे एक व्यक्ति अपना माल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की सहमति से रखता है तो माल की हानि के लिए रेलवे उत्तरदायी होगी।
यह उल्लेखनीय है कि उपनिधान प्रतिफल के बिना तथा संविदा के बिना भी सम्भव है। उपनिधान में वस्तु के कब्जे का अन्तर तथा वस्तु को जिस प्रयोजन के साथ दिया गया है, उस प्रयोजन के पश्चात् लौटाने की शर्त आवश्यक है।
प्रश्न 10. उपनिधाता या निक्षेपक तथा निक्षेपग्रहीता के कर्तव्य (दायित्व) एवं अधिकारों को संक्षेप में बतलाइए।Briefly state duties (Liabilities) and rights of Bailor and Bailee.
उत्तर- उपनिधाता के कर्तव्य (Duties of Bailor) उपनिधान की शर्त के अनुसार, उपनिधाता निःशुल्क या सशुल्क हो सकते हैं। निःशुल्क उपनिधाता के कर्तव्य सशुल्क उपनिधाता से कम होते हैं। जो व्यक्ति अपनी वस्तु का अन्तरण निःशुल्क करता है वह निः शुल्क उपनिधाता है।
उपनिधाता के निम्न कर्तव्य हैं-
(1) वस्तु या माल में निहित त्रुटियों को प्रकट करने का कर्तव्य- संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 150 के अनुसार, उपनिधाता का सबसे प्रथम यह कर्तव्य है कि वह उपनिधान की वस्तु में अन्तर्निहित ऐसी त्रुटियों को प्रकट करे जो उपनिधान के समय उसे ज्ञात थी या जो वस्तु के उपयोग में विघ्न डालने वाली थीं या जिससे उपनिहिती (Bailee) को, खतरा या असाधारण जोखिम में डाले। यदि उपनिधाता ऐसा नहीं करता तो उस त्रुटि से उपनिहिती को होने वाली समस्त क्षतियों के लिए उत्तरदायी होता है।
धारा 150 के द्वितीय पैरा के अनुसार, यदि उपनिधान भाड़े पर (सशुल्क) है तो उपनिधाता त्रुटि से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा भले ही वह माल की त्रुटियों को जानता रहा हो या नहीं।
‘क’ एक ऐसा घोड़ा ‘ख’ को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता था। वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है तथा ‘ख’ को गिरा देता है। ‘ख’ को चोट लगती है। ‘ख’ को लगी चोट (नुकसान) के प्रति ‘क’ उत्तरदायी है।
‘ख’ की गाड़ी ‘क’ भाड़े पर लेता है (सशुल्क उपनिधान) गाड़ी अक्षेमकर है। इस तथ्य की जानकारी ‘ख’ को नहीं है, ‘क’ क्षत हो जाता है। इस क्षति के लिए ‘ख’ उत्तरदायी है।
(2) आवश्यक खर्चों के भुगतान का कर्तव्य – संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 158 के अनुसार, यदि उपनिधान निःशुल्क है तथा उपनिहिती (Bailee) का कोई पारिश्रमिक दिया जाना तय न हो तो उपनिधाता, उपनिहिती को उसके द्वारा उपनिधान के प्रयोजन हेतु वहन किये गये आवश्यक खर्चों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
(3) उपनिधान के समय से पूर्व वस्तु वापस माँगने पर क्षतिपूर्ति का कर्तव्य – संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 159 के अनुसार, यदि उपनिधान निःशुल्क या उधार है तथा किसी निश्चित समय के लिए उपनिधान किया गया है तथा इस निश्चित समय के लिए किये गये उपनिधान के भरोसे उपनिहिती ने कोई ऐसा कार्य किया है कि उपनिधान की गई वस्तु को यदि निश्चित समय से पूर्व वापस ले लिया गया तो उसे लाभ के स्थान पर हानि होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि उपनिधाता उपनिधान की गई या उधार दी गई वस्तु को निश्चित समय से पूर्व वापस ले लेता है तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
(4) उपनिधान करने का अधिकार न होने के कारण होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य- संविदा अधिनियम की धारा 164 के अनुसार, यदि उपनिधाता ने ऐसी वस्तु का उपनिधान किया है जिसे वापस पाने या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लेने हेतु निर्देशित करने का अधिकार उसे नहीं था तो उपनिधाता इस कारण उपनिहिती को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
उपनिधाता (Bailor) के अधिकार- उपनिधाता के निम्न अधिकार हैं-
(1) संविदा अधिनियम की धारा 151 तथा 152 के अनुसार यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई वस्तु के प्रति उतनी सतर्कता या सावधानी नहीं बरतता जितनी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति वैसी वस्तु के प्रति बरतता तो यदि उपनिहिती की असावधानी के कारण उपनिहिती द्वारा वस्तु को कोई क्षति होती है तो उस क्षति को उपनिधाता प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
(2) यदि उपनिहिती (Bailee) उपनिधान की वस्तु को ऐसे प्रयोग करता है जो उपनिधान की शर्त के अनुसार असंगत (incosistant) है तो उपनिधान, उपनिधाता समाप्त करवा सकता है।
(3) संविदा अधिनियम की धारा 154 के अनुसार, यदि उपनिहिती उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक (Unnatural) प्रयोग करता है तथा इस अप्राकृतिक प्रयोग के कारण वस्तु (माल) को कोई क्षति होती है तो उसको क्षतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार उपनिधाता को होगा।
(4) संविदा अधिनियम की धारा 157 के अनुसार, यदि उपनिहिती उपनिधान की हुई उपनिधाता की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रित करता है तो (अ) यदि इस मिश्रण को पृथक् किया जाना सम्भव है तो उसे पृथक् करने में हुए खर्च को उपनिधाता वसूल कर सकता है; (ब) यदि उस मिश्रण का पृथक् किया जाना सम्भव नहीं है तो उपनिधाता उपनिहिती से इस मिश्रण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
(5) संविदा अधिनियम की धारा 160-161 के अनुसार यदि उपनिधान किसौ निश्चित समय के लिए है तथा उपनिधाता द्वारा निश्चित समय के पश्चात् वापस करने की माँग की जाती है तथा उपनिहिती वस्तु को माँगने पर वापस करने में असफल रहता है या यदि उपनिधान निःशुल्क है तथा उपनिधाता द्वारा किसी समय वस्तु वापस माँगने पर उपनिधान की वस्तु उपनिहिती वापस करने में असफल रहता है तो उपनिहिती द्वारा वस्तु वापस न कर पाने के कारण उपनिधाता को जो क्षति होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार उपनिधाता को होगा।
(6) संविदा अधिनियम की धारा 163 के अनुसार, यदि उपनिधान की वस्तु वृद्धि या उससे कोई लाभ उपनिहिती को हुआ है तो उपनिधाता उसे प्राप्त करने का अधिकार रखता है यदि उसके प्रतिकूल उनके मध्य कोई संविदा नहीं हुई है। ‘क’ एक गाय ‘ख’ प की अभिरक्षा में छोड़ता है। गाय को बछड़ा पैदा होता है। ‘ख’ वह बछड़ा ‘क’ को देने के लिए बाध्य है।
उपनिहिती (उपनिधानग्रहीता) (Bailee) के कर्तव्य तथा अधिकार
(क) उपनिहिती (उपनिधानग्रहीता) के कर्तव्य (1) सावधानी बरतने का कर्तव्य- धारा 151 के अनुसार, उपनिहिती का यह कर्तव्य होता है कि उपनिधान की वस्तु के प्रति उचित सावधानी बरते, सतर्कता या सावधानी कितनी होगी इसका स्तर क्या होगा यह स्तर एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति का होगा। इस प्रकार उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधान की वस्तु के प्रति उत्तनी सावधानी बरते जितनी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति प्रश्नगत परिस्थितियों में बरतता है। यह उपनिधान की वस्तु की प्रकृति तथा उसके मूल्य पर निर्भर होगा।
रामपाल बनाम गौरीशंकर, ए० आई० आर० 1952 नागपुर के वाद में उपनिधाता ने उपनिहिती को आभूषण का उपनिधान किया। उपनिहिती ने आभूषण को निचली मंजिल के कमरे में एक सन्दूक में रखकर उसकी ताली उसी कमरे में रख दी। कमरा सुरक्षित नहीं था, आभूषण चोरी हो गये। उपनिहिती अपने कर्तव्य के पालन में सतर्क नहीं था। अतः वह उत्तरदायी पाया गया।
श्री मौर ट्रक आपरेटर्स यूनियन (रजि०) बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, ए० आई० आर० (2011) एन० ओ० सी० 989 हि० प्र० के वाद में एक वाहक बीमा युक्त माल ले जा रहा था। संविदा में खण्ड था कि माल वाहन मालिक के जोखिम पर होगा। चालक की लापरवाही व उतावलेपन के कारण माल की हानि हो गई। निर्णीत हुआ कि वाहक उस हानि के कारण पैदा होने वाले दायित्व से बच नहीं सकता।
विनोद कुमार अग्रवाल बनाम यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, ए० आई० आर० (2015) उत्तराखण्ड 148 के मामले में उपनिहिती के दायित्व का उल्लेख किया गया है। फाइनेन्सियल कारपोरेशन ने भुगतान की चूक करने वाले ऋणी की सम्पत्ति, प्लान्ट, मशीनरी का कब्जा किया-उसकी उचित सुरक्षा न कर पाने पर उसे उत्तरादायी ठहराया गया।
संविदा अधिनियम की धारा 152 यह स्पष्ट करती है कि यदि उपनिहिती ने उचित सावधानी या सतर्कता बरती है तो वह उपनिधान की वस्तु के क्षय या विनाश या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है।
(2) उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक प्रयोग न करने का कर्तव्य- संविदा अधिनियम की धारा 154 के अनुसार उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि उपनिधान की वस्तु का अप्राकृतिक प्रयोग न करे। अन्यथा वह इस अप्राकृतिक प्रयोग से होने वालो क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
‘क’, कलकत्ते में ‘ख’ से एक घोड़ा इस उद्देश्य से उधार लेता है कि वह वाराणसी जाएगा। ‘क’, सम्यक् सवारी करता है वस्तुतः वाराणसी न जाकर कटक चला जाता है। अर्कस्मात् घोड़ा गिर जाता है तथा चोट खा जाता है। ‘क’ घोड़े को हुई क्षति के लिए ‘ख’ को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है।
(3) उपनिधाता की वस्तु का अपनी वस्तु के साथ मिश्रण न करने का कर्तव्य – उपनिहिती (Bailee) का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधाता की वस्तु को उपनिधाता की सहमति के बिना अपनी वस्तु के साथ मिश्रित न होने दे। यदि उपनिहित्ती उपनिधाता की सहमति के बिना उपनिधान की वस्तु को अपनी वस्तु के साथ मिश्रित करता है तो (1) यदि मिश्रण को पृथक् किया जा सकता है तो मिश्रण को पृथक् करने के खर्च को उपनिहिती को वहन करना होगा। यदि (2) मिश्रण पृथक् करने योग्य नहीं है तो वह इस मिश्रण के कारण उपनिधाता को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 156 तथा 157)
‘क’ एक विशिष्ट चिह्न वाली रूई की 10 गाँठें ‘ख’ के पास उपनिधान करता है। ‘क’ की सहमति के बिना ‘ख’ उन गाँठों को एक पृथक् चिह्न वाली अपनी रूई की गाँठों के साथ मिला देता है तो ‘ख’ ‘क’ यदि चाहता है तो, गाँठों को पृथक् करने में लगे व्यय को ‘ख’, ‘क’ को देने के लिए आबद्ध है।
‘क’ 8 रुपये किलो चावल को ‘ख’ के पास उपनिधान करता है। ‘ख’, ‘क’ की सहमति के बिना उस चावल को अपने 5 रुपये किलो वाले मोटे चावल के साथ मिश्रित कर देता है। ‘क’ को उस चावल के मिश्रण के कारण होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने हेतु ‘ख’ बाध्य है।
(4) उपनिधान की वस्तु को वापस देने का कर्तव्य- उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि यदि उपनिधान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए है तो वह प्रयोजन पूरा होने पर तथा यदि उपनिधान एक निश्चित अवधि के लिए है तो उस निश्चित अवधि के पश्चात् उपनिधान की वस्तु को उपनिधाता को वापस कर दे, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह वस्तु की किसी भी क्षति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
‘क’ ने अपनी कुछ पुरु पुस्तकें ‘ख’ को जिल्द चढ़ाने के उद्देश्य से दीं। उचित समय के अन्दर जिल्दसाज को पुस्तकें पुस्तकें वापस करनी थीं। ‘क’ द्वारा उचित समय के अन्दर पुस्तकें वापस माँगने पर ‘ख’ ने पुस्तकें वापस नहीं कीं। जिल्दसाज की दुकान में आग लग जाने से किताबें जलकर नष्ट हो गईं। यद्यपि ‘ख’ की कोई गलती नहीं थी फिर भी उसे क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी माना गया।
(5) उपनिधाता के अधिकार की अवहेलना न करने का कर्तव्य- यदि उपनिधाता अपनी वस्तु वापस माँगता है तो उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि वह (माल) वस्तु वापस करने से इन्कार न करे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 117 के अनुसार उपनिहिती, उपनिधाता के उपनिधान की वस्तु पर हक से इन्कार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि उपनिहिती को उपनिधान की वस्तु का स्वामी कोई अन्य व्यक्ति प्रतीत होता है परन्तु वह वस्तु को उपनिधाता को लौटा देता है तो उसका वस्तु के वास्तविक स्वामी के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।
(6) उपनिधान की वस्तु में उपनिधान की अवधि में हुई क्षति या लाभ लौटाने का कर्तव्य – धारा 163 के अनुसार उपनिधान के दौरान यदि उपनिधान की वस्तु में कोई अभिवृद्धि होती है या कोई लाभ उपनिहिती को होता है तो उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि वह लाभ उपनिधाता को लौटाए।
‘क’, अपनी एक गाय ‘ख’ की अभिरक्षा में छोड़ जाता है। उपनिधान के दौरान गाय बछड़ा देती है। ‘ख’ वह गाय तथा बछड़ा ‘क’ को देने के लिए आबद्ध है।
(ख) उपनिहिती के अधिकार (1) प्रतिकर पाने का अधिकार- संविदा अधिनियम की धारा 164 के अनुसार, यदि उपनिधाता ने ऐसी वस्तु का उपनिधान किया है जिसे वापस पाने का या अन्य व्यक्ति को देने हेतु आदेश देने का अधिकार उसे नहीं था तथा इस कारण उपनिहिती को कोई क्षति होती है तो उसका प्रतिकर पाने का अधिकार उपनिहिती को होगा।
(2) उपनिहिती का खर्च तथा पारिश्रमिक पाने का अधिकार- यदि उपनिधान की संविदा के अन्तर्गत उपनिधाता तथा उपनिहिती के मध्य यह शर्त तय है कि उपनिधाता, उपनिहिती को उपनिधान के लिए कुछ धन देगा तो उपनिहिती उस धन को प्राप्त करने का अधिकार रखता है परन्तु धारा 158 के अनुसार यदि उपनिधाता तथा उपनिहिती के मध्य ऐसा कोई करार या संविदा नहीं है तो उपनिधाता से उपनिहिती उस खर्च को दी की माँग कर सकता है जो उसने उपनिधान के प्रयोजन से आवश्यक रूप से वहन किया है।
सूर्या इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी बनाम एस० टी० सी० ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० (1987) के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारणाधिकार तथा व्यय पाने के अधिकार में अन्तर करते हुए कहा कि धारणाधिकार सिर्फ तब तक ही बना रहता है जब तक वस्तु पर कब्जा बना रहता है। परन्तु धारा 158 के अन्तर्गत व्यय पाने का अधिकार वस्तु पर से कब्जा समाप्त होने के पश्चात् भी प्राप्त होता है।
उपनिहिती अपनी सेवा के लिए, यदि कोई पारिश्रमिक निर्धारित हुआ है तो उसे पाने का अधिकार रखता है।
(3) उपनिहिती का उपनिधान की वस्तु पर धारणाधिकार (Right of Lien)- इस अधिकार का प्रयोग तब होता है जब उपनिहिती को उसके विधिक खर्च उपनिधाता से प्राप्त न हों तथा उपनिधान की वस्तु पर उपनिहिती का कब्जा बरकरार हो। इस अधिकार के अन्तर्गत उपनिहिती जब तक खर्च या पारिश्रमिक न प्राप्त हो वस्तु को अपने कब्जे में रोक सकता है।
किसी वस्तु को उस वस्तु के प्रति खर्च प्राप्त करने के उद्देश्य से रोकने के अधिकार को धारणाधिकार (Right of Lien) कहते हैं।
धारणाधिकार दो प्रकार का होता है-
(i) साधारण धारणाधिकार (General Right of Lien); तथा
(ii) विशिष्ट धारणाधिकार (Particular Lien) 1
(i) साधारण धारणाधिकार (General Right of Lien)- साधारण धारणाधिकार का उल्लेख धारा 171 में किया गया है। इसके अनुसार साधारण धारणाधिकार के अन्तर्गत उपनिहिती को उपनिधाता की कोई भी वस्तु जो उसके पास है, रोकने का अधिकार है भले ही कार्य किसी अन्य वस्तु के सम्बन्ध में हुआ हो। धारा 171 के अनुसार, साधारण धारणाधिकार सिर्फ बैंकर, आढ़तिया, घाटवाल, उच्च न्यायालय के एडवोकेट तथा बीमा दलाल को हो प्राप्त है।
केरल उच्च न्यायालय ने सिन्डीकेट बैंक बनाम विजय कुमार, ए० आई० आर० 1992 एस० सी० 1066 के वाद में दिये गये निर्णय का अनुसरण करते हुए ननकूलाल बनाम डिप्टी जनरल मैनेजर, कनारा बैंक, ए० आई० आर० (2014) केरल 64 के बाद में निर्ण दिया कि बैंक ग्राहक की सावधि जमा पर साधारण धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है और यह सावधि जमा राशि को ग्राहक द्वारा बैंक को देय राशि से समायोजित कर सकता है।
(II) विशिष्ट धारणाधिकार (Particular Lien) – विशिष्ट धारणाधिकार के अन्तर्गत उपनिहिती को सिर्फ उस विशिष्ट वस्तु को रोकने का अधिकार है जिस पर कार्य हुआ है। धारा 170 के अनुसार यदि उपनिहिती ने उपनिहित वस्तु के सम्बन्ध में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार कोई सेवा की है जिसमें श्रम या कौशल का प्रयोग करना था तो उसे उस विशिष्ट वस्तु को तब तक रोकने का अधिकार है जब तक उस सेवा या परिश्रम का मूल्य न मिल जाय परन्तु यदि उसके प्रतिकूल कोई संविदा है तो वह संविदा ही प्रभावी होगी।
इसके अन्तर्गत सुनार, दर्जी या ड्राइक्लीनर वाले को अपनी सेवा का मूल्य प्राप्त होने तक उपनिधान की वस्तु को रोकने का अधिकार है।
(4) वाद या मुकदमा लाने का अधिकार- यदि किसी व्यक्ति ने उपनिधान की वस्तु को उपनिहिती से गलत ढंग से प्राप्त कर लिया है तो धारा 180 उस सामान को वापस पाने हेतु उपनिहिती को उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार देती है।
समस्या- एक साइकिल स्टैण्ड में एक व्यक्ति ने साइकिल बिना ताला लगाये रखी थी, साइकिल गायब हो जाती है। यहाँ स्टैण्ड का ठेकेदार यदि उचित सावधानी या सतर्कता नहीं बरतने का दोषी है तो वह साइकिल के मूल्य के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति साइकिल स्टैण्ड से साइकिल बिना उचित टोकेन या पूछ-ताछ के नहीं ले जाने देगा।
प्रश्न 11. माल पाने वाले के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। Discuss the rights and duties of finder of goods.
उत्तर- जो व्यक्ति किसी खोई या पड़ी हुई वस्तु को प्राप्त करता है वह स्वामी के प्रति उस वस्तु का उपनिहिती हो जाता है। उसे वस्तु के मालिक को ढूँढ़ने तथा वस्तु को सम्भाल कर रखने के कष्ट तथा खर्चों के लिए स्वामी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
धारा 168 के अनुसार-पड़ा माल पाने वाले का अधिकार – पड़ा माल पाने वाले को माल का परीक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छया उठाये गये कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर बाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर न मिल जाए, और यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट, पुरस्कार देने की प्रस्थापना की हो तो पड़ा माल पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा और माल को तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे वह पुरस्कार न मिल जाए।
सामान्य विधि के अनुसार पड़ी हुई वस्तु को पाने वाले व्यक्ति का स्वत्व (Title) वास्तविक स्वामी को छोड़कर समस्त लोगों के विरुद्ध मान्य होता है।
यदि वस्तु कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत निवास पर पाता है तो स्थिति-जैसे विश्वविद्यालय के प्रांगण में पायी हुई वस्तु का स्वामित्व विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय एक विधिक व्यक्ति होता है। प्राप्त होता है; क्योंकि अगर यह वस्तु सार्वजनिक स्थान पर पायी जाय तो वास्तविक स्वामी के अलावा स्वामित्व पाने वाले व्यक्ति का ही होगा।
इसके सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं-
(1) वस्तु को पाने वाला व्यक्ति. वास्तविक स्वामी के विरुद्ध उस वस्तु को सुरक्षित रखने, सावधानी बरतने, मालिक का पता लगाने में हुई परेशानियों एवं खर्चे को प्राप्त नहीं कर सकता है तथा किये गये खर्च के लिए माल भी रोक नहीं सकता है। विन्सटेड बनाम वक, 96 ई० आर० 660 के वाद में एक व्यक्ति ने खोये हुए कुत्ते को 20 सप्ताह तक खाना खिलाया और इसके लिए 20 शिलिंग माँगे। न्यायालय ने कहा कि अपने खचों को प्राप्त करने के लिए न तो वह वाद ला सकता था और न कुत्ते को रोक सकता था।
(2) प्रतिकर न प्राप्त हो जाने तक वह उस वस्तु को अपने पास रख सकता है, क्योंकि वस्तु को पड़ी हुई पाने मात्र से उसका धारणाधिकार (Lien) कायम हो जाता है।
(3) जब वास्तविक स्वामी ने कोई इनाम घोषित किया है तो पाने वाला व्यक्ति उसकी प्राप्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। वह वस्तु को तब तक अपने अधिकार में रख सकता है जब तक उसे इनाम प्राप्त न हो जाए।
धारा 169-सामान्यतया विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा – जबकि कोई चीज, जो सामान्यतया विक्रय की विषय हो, खो जाय तब यदि स्वामी का युक्तियुक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके या यदि वह पड़ा पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों का माँगे जाने पर संदाय करने से इन्कार करे तो पड़ा पाने वाला उसको बेच सकेगा-
(1) जबकि उस चीज के नष्ट हो जाने या उसके मूल्य का अधिकांश भाग जाते रहने का खतरा हो; अथवा
(2) जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़े पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य की दो-तिहाई तक पहुँच जाए।
इस धारा में वस्तु को पाने वाले व्यक्ति के विक्रय करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है जो निम्न परिस्थितियों में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जब-
(i) पायी गई वस्तु विक्रय की जाने वाली हो; या
(ii) वस्तु के वास्तविक स्वामी का पता न चल पाया हो; या
(iii) वस्तु के नष्ट होने का भय हो;
(iv) वस्तु के मूल्य का अधिकतम भाग कम होने की आशा हो;
(v) पाने वाले व्यक्ति का प्रभार (Charge) वस्तु के मूल्य का दो-तिहाई हो;
(vi) वास्तविक स्वामी का पता लग गया हो, लेकिन प्रभार (Charge) न दिया गया हो।
गिरवी (Pledge)
(धाराएँ 127 से 179)
प्रश्न 12. (क) गिरवी को परिभाषित कीजिए। गिरवी के आवश्यक तत्व क्या हैं? Define Pledge. What are the essential elements of Pledge?
(ख) गिरवी कौन कर सकता है और कौन नहीं? विवेचना कीजिए। Who can make a valid pledge and who cannot make a valid pledge? Explain this principle.
उत्तर (क)- गिरवी (Pledge)- गिरवी एक ऐसा उपनिधान है जिसके अन्तर्गत वस्तु का परिदान ऋण की प्रत्याभूति के रूप में किया जाता है। लेनदार वस्तु को प्राप्त करता है और उसे सुरक्षित रखता है और वस्तु का अधिकार उसी व्यक्ति में निहित रहता है। संविदा अधिनियम की धारा 172 गिरवी की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली, ए० आई० आर० (1967) एस० सी० 1322 के बाद में गिरवी को परिभाषित किया गया है कि “गिरवी किसी माल का उपनिधान है जो किसी ऋण या संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है।”
एक वैध गिरवी की परिभाषा में मुख्य दो बातें सामने आती हैं कि-
(1) वस्तु का (माल का) उपनिधान होना चाहिए।
(2) वस्तु का उपनिधान ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन के प्रतिभूति के लिए होना चाहिए।
(1) वस्तु का उपनिधान- गिरवी एक चल सम्पत्ति की ही हो सकती है जिसके कब्जे का अन्तरण पणयमकार (गिरवीदाता) द्वारा गिरवीग्रहौता (पणयमदार) को आसानी से हो सके। गिरवी में वस्तु का परिदान अर्थात् वस्तु के कब्जे का अन्तरण होना आवश्यक है। वस्तु का परिदान वास्तविक (Actual) या विवक्षित (constructive) दोनों प्रकार से हो सकता है। जब वस्तु का वास्तविक परिदान (अन्तरण) तो नहीं है परन्तु पणयमदार द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे वस्तु पर कब्जा पाने का अधिकार पणयमदार (गिरवीग्रहीता) (Pawnee) को प्राप्त हो जाता है। जैसे- वस्तु से सम्बन्धित रेलवे रसीद या बिल्टी या उस गोदाम की चाभी पणयमग्रहीता को दे देना जिसमें वस्तु रखी गई है, विवक्षित परिदान कहा जा सकता है।
यदि एक व्यक्ति का माल किसी अन्य व्यक्ति के पास पणयम की संविदा से पूर्व है तब बाद में माल का. स्वामी उससे पणयम (गिरवी) की संविदा करता है तो उस संविदा के पश्चात् जिसके कब्जे में माल पहले से है, वह पणयमदार हो जाता है।
रेवेन्यू प्राधिकारी बनाम सुदर्शन पिक्चर्स, ए० आई० आर० (1968) मद्रास के वाद में एक फिल्म-निर्माता ने वितरक से ऋण लेने की संविदा की तथा यह सहमति हुई किं जैसे हो फिल्म तैयार होगी वह वितरक को गिरवी के रूप में दे दी जायेगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे गिरवी नहीं माना क्योंकि गिरवी की संविदा के समय गिरवी की वस्तु का अस्तित्व नहीं था तथा माल के अन्तरण के अभाव में यह संविदा गिरवी की संविदा नहीं मानी जा सकती। कभी-कभी ऐसा होता है क गिरवीदार माल किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए गिरवीकर्ता के पास ही रहने देता है तो भी यह विधिमान्य गिरवी माना जायेगा। जैसे बैंक ऑफ चित्तूर बनाम नरसिम्बुल, ए० आई० आर० (1966) आन्ध्र प्रदेश 163 में एक सिनेमा प्रोजेक्टर बैंक के पास ऋण लेने हेतु गिरवी रखा गया परन्तु प्रोजेक्टर गिरवी करने वाले के पास ही रहने दिया गया जिससे कि प्रोजेक्टर का प्रयोग होता रहे। उच्चतम न्यायालय ने उसे विधिमान्य गिरवी माना।
(2) वस्तु का उपनिधान ग्रहण के भुगतान या किसी वचन पालन के प्रतिभूति के लिए – यही तथ्य उपनिधान तथा गिरवी में अन्तर प्रकट करता है। उपनिधान में वस्तु का अन्तरण ऋण लेने के प्रयोजन के लिए होता है तथा जब यह प्रयोजन ऋण लेना या किसी वचन के पालन के प्रतिभूति देना होता है तो वे उपनिधान, गिरवी का रूप ले लेते हैं। ऋण का भुगतान या वचन पालन हो जाने के पश्चात् गिरवी की वस्तु गिरवीकर्ता (पणयमकार) (Pawnee) को वापस लौटा दी जाती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि ऋण लेने तथा गिरवी हेतु माल के अन्तरण का कार्य एक साथ हो। गिरवी की संविदा में जो व्यक्ति गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करता है, उसे पणयमकार या गिरवीदार (Pawner) कहते हैं तथा जो व्यक्ति माल अपने नियन्त्रण में रखकर ऋण लेता है उसे पणयमदार या गिरवीग्रहीता (Pawnee) कहते हैं।
गिरवी के आवश्यक तत्व – एक वैध गिरवी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं-
(1) चल सम्पत्ति होनी चाहिए- गिरवी केवल चल सम्पत्ति की हो सकती है। अचल सम्पत्ति की नहीं।
(2) सम्पत्ति का कब्जा- गिरवी के लिए आवश्यक है कि गिरवी की सम्पत्ति पर कब्जा होना चाहिए परन्तु गिरवी की सम्पत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। वस्तु का कब्जा वास्तविक या विवक्षित रूप से दिया जा सकता है। [सुनील कुमार गुप्ता बनाम पंजाब और सिन्ध बैंक, ए० आई० आर० (2006) उत्तरांचल] किसी गोदाम की कुंजी कुंजी प्रदान करना, किसी माल की बिल्टी देना या किसी माल का स्वत्व सम्बन्धी प्रलेख दिया जाना कब्जा दिये जाने के समतुल्य होता है। कभी-कभी गिरवी रखने के बाद किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु माल पणयमकार की अभिरक्षा में छोड़ दिया जाता है तब भी गिरवी की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
मर्केन्टाइल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (1938) के मामले में माल की बिल्टियों को गिरवी रखे जाने के बाद उसे छुड़ाकर वापस ले लेने से गिरवी नष्ट नहीं होती है; मद्रास उच्च न्यायालय ने एक वाद में विचार व्यक्त किया कि यदि गिरवी रखी गयी मोटर गाड़ियाँ पणयमकार के प्रदर्शन कक्ष में रहने दी जायँ तो भी गिरवी मान्य होगी। इसी प्रकार न्यायिक निर्णयों के आधार पर रचनात्मक कब्जे के बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं।
(3) संविदा के अन्तर्गत होनी चाहिए- गिरवी में वस्तुओं का परिदान ऋण के अन्तर्गत होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कार्य एक ही समय हों। इन परिस्थितियों में गिरवी मान्य होती है।
(4) ऋण के लिए – वस्तुओं का परिदान ऋण के लिए या प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए होना चाहिए।
(5) प्रतिभूति के रूप में- जब माल का परिदान ऋण के भुगतान के लिए या प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में होता है, तो इसे गिरवी कहते हैं।
(6) वस्तु को रखने का अधिकार- गिरवी रखी गयी वस्तुएँ गिरवी ग्राही या पणयमदार के कब्जे में तब तक रहती हैं, जब तक कि ऋण का भुगतान न हो जाय।
उत्तर (ख)- गिरवी कौन कर सकता है- जिस व्यक्ति को माल का स्वामित्व प्राप्त होता है, वही व्यक्ति गिरवी रख सकता है या उसके द्वारा अधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा गिरवी रखा जा सकता है। एक मामले में नौकर द्वारा रखी गयी गिरवी नहीं मानी गयी।
इस प्रकार सामान्य नियम के अनुसार माल की गिरवी उसके स्वामी अथवा स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं अर्थात् कुछ दशाओं में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी गिरवी विधिपूर्ण होती है जो गिरवी किये गये माल का न तो स्वामी होता है और न तो स्वामी द्वारा गिरवी करने के लिए अधिकृत होता है यद्यपि वह स्वामी की सम्मति से माल पर कब्जा प्राप्त करता है। इसका प्रावधान धारा 178, 178-क, एवं 179 इत्यादि धाराओं में किया गया है-
धारा 178-वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी – जहाँ कि कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की सम्मति से माल पर या माल के हक के दस्तावेजों पर कब्जा रखता है वहाँ वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी ही विधिमान्य होगी जैसे वह माल के स्वामी द्वारा कार्य करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो परन्तु यह तब जबकि पणयमदार सद्भावपूर्वक कार्य करें और गिरवी के समय से यह सूचना न हो कि पणयमकार गिरवी करने का प्राधिकार नहीं रखता।
(2) धारा 178-क-शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी- जबकि पणयमकार ने अपने द्वारा गिरवीकृत माल का कब्जा धारा 19 या 19- क के अधीन शून्यकरणीय किसी संविदा के अधीन अभिप्राप्त किया हो किन्तु संविदा गिरवी के समय विखण्डित न हो चुकी हो, तो पणयमदार उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है परन्तु यह तब जबकि वह सद्भावपूर्वक और पणयमकार के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करे।
इस धारा के लागू होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं-
(i) गिरवीकर्ता ने वस्तुओं को कपट, मिथ्याव्यपदेशन, असम्यक असर तथा उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की हो;
(ii) गिरवी किये जाने के पूर्व संविदा विखण्डित न की गयी हो;
(iii) गिरवीग्राही ने सद्भावपूर्वक गिरवीकर्ता के स्वत्व की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य किया हो यदि माल ऐसी संविदा के अन्तर्गत लिया गया है जो शून्य है तो ऐसे माल को गिरवी नहीं रखा जा सकता।
(3) धारा 179-जहाँ परिसीमित हित हो- इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने सीमित हित को भी गिरवी रख सकता है जो उस हित की सीमा तक मान्य होगी जैसे-
ठाकुर दास बनाम मथुरादास, ए० आई० आर० 1958 इलाहाबाद 66 के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब पणयमदार माल को गिरवी रख दे तो उसके हित की सीमा तक ही गिरवी मान्य होगी। उसका हित केवल उस धन तक है जितने पर कि उसका माल गिरवी रखा गया है। उदाहरणार्थ ‘क’ एक हजार रुपये के लिए अपना माल ‘ख’ के पास गिरवी रखता है। ‘ख’ उस माल को अपने हित की सीमा तक किसी अन्य व्यक्ति को गिरवी रख सकता है। यदि वह उससे अधिक के लिए गिरवी रखता है तो भी ‘क’ ने जितनी रकम के लिए ‘ख’ के पास गिरवी रखा है उतनी रकम देकर माल वापस ले सकता है।
गिरवी कौन नहीं कर सकता- निम्न व्यक्ति गिरवी नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा की गयी गिरवी मान्य नहीं होगी-
(1) पत्नी अपने पति के जेवरात की उनकी तरफ से अभिरक्षक है;
(2) नौकर जिसे मालिक ने अपनी अनुपस्थिति में माल सुपुर्द किया है;
(3) व्यक्ति जिसे माल भाड़े पर दिया गया है।
प्रश्न 13. (क) गिरवीग्रहीता (पणयमदार) एवं गिरवीकर्ता (पणयमकार) के अधिकारों का उल्लेख करें। Give the rights of Pawnee and Pawnor.
(ख) वस्तु के मालिक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा गिरवी रखना किन दशाओं में वैध है? गिरवी व बन्धक में अन्तर को स्पष्ट कीजिए। When can a pledge made by non-owner of goods be valid? What is difference between pledge and mortgage.
उत्तर (क)- गिरवीग्रहीता या पणयमदार के अधिकार- एक पणयमदार या गिरवीग्रहीता के निम्न अधिकार हैं-
(1) प्रतिधारण का अधिकार (धारा 173);
(2) असामान्य खचों को पाने का अधिकार (धारा 175);
(3) वस्तु (माल) बेचने का अधिकार (धारा 176)।
(1) पणयमदार या गिरवीग्रहीता का प्रतिधारण का अधिकार (धारा 173 एवं174) – पणयमदार या गिरवीग्रहीता का महत्वपूर्ण अधिकार है कि जब तक उसके ऋण का भुगतान न किया जाय वह गिरवी के माल को रोककर रख सकता है। ऐसा वह सिर्फ ऋण हो नहीं परन्तु ऋण का ब्याज तथा अन्य सामान्य खर्चों की अदायगी न होने तक कर सकता है। पणयमदार सिर्फ उसी वस्तु को रोके रख सकता है जिसके बदले में ऋण लिया गया है तथा संविदा के अभाव में वह अन्य माल को नहीं रोक सकता।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०, ए० आई० आर० (2015) एन० ओ० सी० 423 (इला०) के बाद में निश्चित किया गया कि वित्तीय संस्थाओं का अधिकार-गन्ना उत्पादकों के अधिकार पर अधिभावी होगा? चीनी मिल ने चीनी स्टॉक को प्रतिभूति रखकर ऋण लिया जिसका भुगतान गन्ना उत्पादकों को दिया जाना था। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाएं पणयमदार के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं।
धारा 174 के अनुसार, यदि एक व्यक्ति अपना माल गिरवी रखकर कोई ऋण लेने के पश्चात् पुनः गिरवीग्रहीता से ऋण लेता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह उत्तरवर्ती ऋण भी उस माल के ऊपर लिया गया है। जैसे ‘अ’, ‘ब’ से अपनी कार गिरवी रखकर 25,000 रुपये ऋण लेता है। उस ऋण के पश्चात् वह ‘ब’ से 15 हजार और ऋण लेता है। यह माना जायेगा कि वह 15 हजार उसी कार के गिरवी के आधार पर लिया गया है।
गिरवीग्रहीता को गिरवी रखे गये माल पर एक विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है जहाँ स्वामित्व तो पणयमकार के पास रहता है परन्तु अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गिरवीग्रहीता के पास भी एक विशेष प्रकार का स्वामित्व रखता है।
(2) गैर मामूली खर्चों को प्राप्त करने का अधिकार- गिरवीग्रहीता यदि गिरवीग्रस्त माल को सुरक्षित रखने में कोई खर्च या व्यय करता है तो धारा 175 उसे अधिकार देती है कि वह उन गैर मामूली खर्चों को पणयमकार (गिरवीकर्ता) से प्राप्त करने क अधिकार रखता है।
(3) वस्तु या माल को बेचने का अधिकार- संविदा अधिनियम की धारा 176 पणयमदार या गिरवीग्रहीता को दो अधिकार उन परिस्थितियों में प्रदान करते हैं जब पणयमकार त्रऋण का भुगतान न करे।
प्रथम तो यह कि वह ऋण के भुगतान के लिए वाद करे तथा माल को उस दौरान प्रतिभूति के रूप में अपने कब्जे में रोके रखें। दूसरा यह कि वह पणयमकार (Pawnor) को उचित सूचना देकर माल को बेच भी सकता है। गिरवी रखे गये माल को ऋण का भुगतान होने तक रखा जा सकता है तथा ऋण का भुगतान होने के पश्चात् ही उसे छोड़ देना पड़ेगा। परन्तु यदि गिरवीग्रहीता माल को लौटाने में असमर्थ है तो वह ऋण के लिए वाद लाने का अधिकारी नहीं है।
लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली, ए० आई० आर० 1967 सु० को० 1322 के वाद में प्रतिवादी ने 35,000 रुपये की कीमत का हवाई जहाज का ऐयरोस्क्रेप्स गिरवी रखकर 20,000 रुपये का ऋण लिया। वादी ने उस वस्तु को बेच दिया तत्पश्चात् ऋण की अदायगी का वाद चलाया जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि गिरवी-ग्रहीता माल लौटाने में असमर्थ था।
यदि समय के पश्चात् पणयमकार (Pawnor) के भुगतान में असफल रहता है तो पणयमदार (गिरवीग्रहीता) को यह अधिकार है कि वह गिरवीग्रस्त माल को बेच दे परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि माल के विक्रय से पूर्व पणयमकार (Pawnor) को इस बात की उचित सूचना अवश्य दी जाय।
सुन्दर लाल सर्राफ बनाम सुभाष चन्द्र जैन, ए० आई० आर० (2006) एम० पी० 35 के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि गिरवीकर्ता निश्चित अवधि के अन्तर्गत ब्याज सहित ऋण वापस नहीं करता, गिरवीग्रहीता गिरवी किये गये माल को बेचने के आशय से सूचना देता है। तत्पश्चात् भी ऋण का भुगतान न करके मात्र विक्रय स्थगित करने की सूचना देता है। तत्पश्चात् गिरवीग्राही विक्रय स्थगित न करके माल का विक्रय कर देता है तो यह विधि विरुद्ध नहीं होगा।
इस प्रकार उचित सूचना देकर गिरवीग्राही गिरवी की गई वस्तु का विक्रय कर सकता है।
पणयमकार या गिरवीकर्ता (Pawnor) के अधिकार (धारा 17)
(1) माल छुड़ाने का अधिकार- पणयमकार को ऋण का भुगतान करके माल को वापस पाने का पूरा अधिकार है। माल वापस पाने का अधिकार उस समय तक बना रहता है जिस तिथि को माल बेच देने की सूचना पणयमदार या गिरवीग्रहीता ने निर्धारित किया है। परन्तु धारा 170 के अनुसार माल वापस पाने (छुड़ाने) का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक माल वास्तव में बेच न दिया गया हो, माल छुड़ाने का अधिकार सूचना में निर्धारित समय से नष्ट नहीं होता। यह माल के वास्तविक विक्रय (Actual sale) के समय तक बना रहता है तथा वास्तविक विक्रय पर समाप्त हो जाता है। यदि माल सूचना में अंकित तिथि के पश्चात् छुड़ाया जाता है तो पणयमकार वीच के समय के खर्च को वहन करेगा।
(2) गिरवी काल में वस्तु में हुई वृद्धि को पाने का अधिकार- यदि गिरवी काल में गिरवीग्रस्त माल में कोई अभिवृद्धि होती है तो उस अभिवृद्धि को पाने का अधिकार पणयमकार को होता है। जैसे ‘क’, अपने अंश तथा शेयर गिरवी रखकर ‘ब’ से ऋण प्राप्त करता है। गिरवी काल में अंश तथा शेयर के दामों में वृद्धि होती है। पणयमकार (Pawnor) इस वृद्धि को पाने का अधिकार रखता है।
उत्तर (ख)- साधारणतः माल का स्वामी ही अपने माल की वैध गिरवी रख सकता है तथा अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के माल को गिरवी रखना अवैध होगा, परन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में वे व्यक्ति जो माल के स्वामी या मालिक नहीं हैं, भी अन्य व्यक्तियों के माल की वैध गिरवी रख सकते हैं, यदि उनका माल के साथ किसी तरह का व्यापारिक सम्बन्ध है तथा गिरवी रखते समय माल उनके अधिकार में है। निम्न व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को माल गिरवी रखना वैध होगा-
(1) व्यापारिक एजेण्ट द्वारा गिरवी (Pledge by mercantile agent) व्यापार की साधारण प्रगति में एक व्यापारिक एजेण्ट की तरह कार्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई माल अथवा माल के अधिकार पत्र हैं, जो कि स्वामी की सहमति से उसे प्राप्त हुए हैं, तो वह एक व्यापारिक एजेण्ट की स्थिति में स्वामी के माल एवं प्रपत्र गिरवी रख सकता है और यह गिरवी पूर्ण रूप से वैध होगी, यदि गिरवी रख लेने वाले ने सद्भाव से कार्य किया है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि गिरवी रखने वाले को माल को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, जैसे कि कमीशन एजेण्ट अथवा दलाल (Broker) द्वारा माल को गिरवी रखना हो तो भी गिरवी वैध होगी। (धारा 178)
(2) व्यर्थनीय अनुबन्ध के अधीन अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा गिरवी (Pledge by person in possession of goods under voidable contracts) अधिनियम की धारा 19 एवं 19-A के अधीन उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट एवं मिथ्यावर्णन के अधीन माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध निरस्त किये जाने से पूर्व भी माल की गिरवी वैध होगी और गिरवी रख लेने वाला माल पर वैध अधिकार प्राप्त कर लेता है, यदि उसने सद्भाव से कार्य किया है एवं उसे गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति के स्वत्व सम्बन्धी दोष की जानकारी नहीं थी। [धारा 178-(A)]
(3) माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी (Pledge by a person having limited Interest) किसी माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा भी माल गिरवी उसके हित की सीमा तक वैध होगी, यद्यपि वह माल का स्वामी नहीं। उदाहरण-‘अ’ को रास्ते में एक गाय मिली जो कि बीमार थी, वह उसे घर ले जाता है एवं उसके इलाज पर 50 रुपये व्यय करता है। गाय के ठीक हो जाने पर वह गाय को 200 रुपये में ‘ब’ के पास गिरवी रख देता है। गाय का वास्तविक स्वामी 50 रुपये ‘ब’ को देकर माल वापस ले सकता है। (धारा 179)
(4) सह-स्वामी द्वारा गिरवी (Pledge by co-owners) – एक ही वस्तु के विभिन्न सह-स्वामी होने की दशा में यदि वस्तु अन्य सह-स्वामियों की सहमति से किसी एक के अधिकार में है तो ऐसा व्यक्ति उस माल की वैध गिरवी रख सकता है, यदि गिरवी रख लेने वाले ने सद्भाव से कार्य किया है तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त व्यक्ति को माल पर पूर्ण स्वामित्व नहीं प्राप्त है। [वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 28]
(5) विक्रय के बाद विक्रेता द्वारा गिरवी (Pledge by a seller in possession after sale)- ऐसा विक्रेता जिसके पास वस्तु विक्रय हो जाने के पश्चात् भी माल अथवा माल के अधिकार पत्र हैं, उसके अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यापारिक एजेण्ट के द्वारा उक्त माल की गिरवी वैध होगी, यदि गिरवी रखने वाले ने सद्विश्वास से कार्य किया है एवं उसके विक्रय व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं था।
(6) विक्रय के पूर्व क्रेता द्वारा बिक्री (Pledge by a buyer in possession of 2001 before sale is completed) – यदि वस्तु के विक्रय पूर्ण होने से पूर्व ही विक्रेता की सहमति से क्रेता ने माल पर अधिकार कर लिया है तो उसके द्वारा माल की गिरवी वैध होगी, यदि गिरवी रख लेने वाले ने सद्विश्वास से कार्य किया है और उसे पिछले व्यवहार की जानकारी नहीं है।
संविदा अधिनियम की धारा 180 के अनुसार, यदि कोई तीसरा व्यक्ति दोषपूर्ण रूप से निक्षेपग्रहोता को निक्षेप किये गये माल के प्रयोग अथवा अधिकार से वंचित करता है अथवा हानि पहुँचाता है तो निक्षेपग्रहीता माल के स्वामी के समान उपचार प्रयोग में ला सकता है, जैसे कि माल का निक्षेप ही न किया गया हो एवं निक्षेपी अथवा निक्षेपग्रहीता कोई भी ऐसे तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार अथवा प्रयोग की रुकावट के विरुद्ध दावा दायर कर सकता है। वाद के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि को निक्षेपी एवं निक्षेपग्रहीता के बीच उनके हितों के अनुसार बाँटा जायेगा। (धारा 180-181)
गिरवी व बन्धक में अन्तर
(Difference between Pledge and Mortgage)
(1) गिरवी, ऋण के लिए या ऋण की अदायगी या प्रतिज्ञा पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में उपनिधान है। जबकि बन्धक एक उल्लिखित सम्पत्ति में हित के अन्तरण को कहते हैं. जिसमें अग्रिम रूप में दिये गये या कर्ज में दिये जाने वाले धन की वापसी अथवा भावी कर्ज को प्रतिभूति प्रदान की जाती है।
(2) गिरवी में साधारणतया वस्तु का कब्जा दिया जाता है। जबकि सादे बन्धक में बन्धकी को बन्धक की गई सम्पत्ति का कब्जा न सौंपकर बन्धककर्ता का ही कब्जा बना रहता है।
(3) गिरवी में धन की अदायगी न होने पर गिरवीग्राही पणयमकार को सम्यक् नोटिस देने के उपरान्त वस्तुओं को बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। जबकि बन्धकी बन्धकित सम्पत्ति को बेच देने का अधिकार रखता है।
अभिकरण (Agency)
(धाराएँ 182-210)
प्रश्न 14. अभिकरण की परिभाषा दीजिए। अभिकरण स्थापित करने के विभिन तरीकों का वर्णन कीजिए।
Define Agency? Discuss the different modes for creation of Agency?
उत्तर- अभिकरण की परिभाषा अभिकरण दो व्यक्तियों के मध्य स्थापित एक सम्बन्ध है जिसमें एक व्यक्ति जिसे मालिक कहते हैं. अभिव्यक्त या विवक्षित रूप में सहमति देता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सहमति देते हुए उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करता है।
ऐन्सन (Anson) महोदय के अनुसार, “यद्यपि सामान्य नियम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके किसी तीसरे व्यक्ति को न तो अधिकार दे सकता है और न सो उत्तरदायित्व अधिरोपित कर सकता है परन्तु नियोजन किये जाने पर यह उस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्षकार से विधिक सम्बन्ध स्थापित करे। इस उद्देश्य के नियोजन को अधिकरण कहते हैं।”
महेश चन्द्र वसु बनाम तिलकराम, ए० आई० आर० (1938) नागपुर 254-255 के बाद में अभिकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-
“एक अधिकर्ता अपने स्वाधी से, दूसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक सम्बन्ध उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करता है” वह शक्ति ही अभिकरण का मुख्य तत्व है।
यू० टी० आई० बनाम रविन्द्र कुमार शुक्ला, ए० आई० आर० (2005) एस० सी० 3528 के मामले में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (यू० टी० आई०) ने एक चेक पंजीकृत डाक द्वारा, आदाता (Payee) को भेजा, परन्तु आदाता को वह चेक प्राप्त नहीं हुआ। आदाता व यू० टी० आई० के मध्य डाक से चेक भेजे जाने के सम्बन्ध में कोई संविदा नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पोस्ट ऑफिस यू० टी० आई० के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। चेक न पहुँचने का दायित्व पोस्ट ऑफिस का न होकर यू० टी० आई० का होगा।
अभिकरण के आवश्यक तत्व –
(i) अभिकरण के लिए दो व्यक्तियों के मध्य सम्बन्ध का वर्तमान रहना आवश्यक है।
(ii) एक व्यक्ति, जिसे स्वामी कहते हैं, वह अपनी सहमति दे कि दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व या उसके बदले में कार्य करे।
(iii) दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति देता है।
एक मान्य अभिकरण के निम्न मुख्य तत्व होते हैं-
(i) स्वामी संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
(ii) कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है।
(iii) अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। (धारा 185)
अभिकरण स्थापित करने के विभिन्न तरीके – एन्सन महोदय ने अभिकरण की स्थापना के पाँच तरीकों का उल्लेख किया है, जिसका प्रावधान धाराओं में भी किया गया है-
(1) स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार द्वारा;
(2) अनुसमर्थन द्वारा;
(3) दृश्यमान प्राधिकार द्वारा;
(4) आवश्यकता द्वारा; तथा
(5) विबन्ध द्वारा अभिकरण।
(1) स्वामी के अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार द्वारा – कोई भी व्यक्ति स्वामी की इच्छा के बिना उसका अभिकर्ता नहीं हो सकता इसलिए अभिकरण का निर्माण संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में नियोजित करके किया जाता है। एक अवयस्क व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता परन्तु वह अभिकर्ता के रूप में नियोजित किया जा सकता है। अभिव्यक्त नियोजन का अर्थ यह है कि जब नियोजन लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा होता है तो उसे अभिव्यक्त नियोजन कहते हैं. जिसके अन्तर्गत अभिकर्ता को दिये गये प्राधिकार भी लिखित या मौखिक होते हैं, जिसके आधार पर नियुक्त व्यक्ति कार्य करता है या मालिक का प्रतिनिधित्व करता है। जो कार्य अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक की ओर से किया जाता है और उसके प्राधिकार क्षेत्र में होता है वह मालिक पर बन्धनकारी होता है।
कभी-कभी पक्षकारों के आचरण या परिस्थिति, सम्बन्धों से भी अभिकरण की स्थापना होती है। जब किसी व्यक्ति के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका अभिकर्ता है तो उसके मध्य विवक्षित अभिकरण का निर्माण हो जाता है।
पति-पत्नी के मध्य विवक्षित आचरण के माध्यम से पति-पत्नी के आस-पास रहने पर उनके बीच विवक्षित अभिकरण स्थापित हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि पति ने पत्नी के घरेलू वस्तुओं को क्रय करने का प्राधिकार दिया है और इस हेतु उधार ली गयी वस्तुओं के मूल्य के भुगतान के लिए दायी होता है।
(2) अनुसमर्थन द्वारा- जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए, उसकी सहमति या ज्ञान के बिना कोई कार्य करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्राप्त होता है। यदि वह उस कार्य की पुष्टि या अनुसमर्थन कर दें तो यह मान लिया जायेगा कि कार्य उसकी सहमति, ज्ञान या प्राधिकार से किया गया है। इस प्रकार अनुसमर्थन का अर्थ बिना अधिकार से किये गये कार्यों को स्वीकार करना होता है।
जैसे-‘क’, ‘ख’ के प्राधिकार के बिना उसके लिए वस्तुएँ खरीदता है, तत्पश्चात् ‘ख’ अपने एकाउण्ट से ‘ग’ को विक्रय कर देता है। यहाँ पर ‘ख’ का यह व्यवहार ‘क’ द्वारा किये गये कार्य का अनुसमर्थन करता है।
(3) दृश्यमान प्राधिकार द्वारा अभिकरण- जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से, तीसरे व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि उस प्रकार के कार्य एवं दायित्व अभिकर्ता के प्राधिकार की सीमा में थे, तब यह अभिकर्ता प्राधिकार के बिना अपने मालिक के लिए तीसरे व्यक्ति के प्रति जो कार्य करता है या दायित्व निभाता है तो उस कार्य या दायित्व से मालिक बाध्य होगा। यह दायित्व किसी वास्तविक प्राधिकार पा आधारित नहीं है बल्कि विबन्ध द्वारा आरोपित होते हुए दृश्यमान प्राधिकार के अन्तर्गत आता है।
दृश्यमान प्राधिकार विबन्ध के सिद्धान्त का उपयोग है। इस सिद्धान्त के अनुसार वा व्यक्ति उन कार्यों एवं संव्यवहार के लिए उत्तरदायी हो सकता है जो कार्य उसके अभिव्यका व विवक्षित प्राधिकार या अनुसमर्थन के बिना हुआ है।
(4) आवश्यकता द्वारा उत्पन्न अभिकरण – आवश्यकता का अभिकरण विद्यमान अभिकरण में उत्पन्न होता है और ऐसी अनपेक्षित घटनाओं में लागू होता है जिनका प्रावधार अभिकरण की संविदा में न हो। इससे सम्बन्धित वाद सिम्स एण्ड कम्पनी बनाम मिड लैण्ड रेलवे कम्पनी, (1913) 1 के० वी० 103 के मामले में रेलवे कम्पनी को कुछ मक्खन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए सुपुर्द किया। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उक्त सामान रास्ते में ही रुक गया। माल की प्रकृति नाशवान होने के कारण कम्पनी ने उसे बेच दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मालिक विक्रय से बाध्य था क्योंकि ऐसा करना उस परिस्थिति में आवश्यक था।
(5) विबन्ध द्वारा स्थापित अभिकरण – यह आचरण द्वारा उत्पन्न अभिकरण के अन्तर्गत स्थापित होता है। जब कोई व्यक्ति आचरण द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपना अभिकर्ता होने का प्रदर्शन करने देता है तथा तीसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके उससे संव्यवहार करता है तो प्रदर्शन करने देने वाला व्यक्ति ऐसा करने से विबन्धित कर दिया जायेगा कि वह अभिकर्ता उसका अभिकर्ता नहीं था। अमेरिकी बाद जॉनसन बनाम मिलवान्की, (1895) 46, नेव 480 के बाद में विबन्ध के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है-जब मालिक अपने अभिकर्ता को ऐसी स्थिति धारण करने देता है कि कोई भी साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति यह समझकर कि अभिकर्ता को कोई विशेष कार्य करने का प्राधिकार है, ऐसा करने का संव्यवहार अभिकर्ता से कर लेता है तो ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रति मालिक विबन्ध से बाध्य होगा और वह यह नहीं कह सकता है कि अभिकर्ता को ऐसा कार्य करने का प्राधिकार नहीं था।”
विबन्ध द्वारा स्थापित अभिकरण का उदाहरण- काशीनाथ बनाम निशाकर रावत, ए० आई० आर० 1962 उड़ीसा 164 के वाद में स्पष्ट होता है कि भूस्वामी द्वारा तहसीलदार को भूमि का प्रबन्धक नियुक्त किया गया, जिसे उस भूमि को किराये पर उठाने का प्राधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार ने भूमि को किराये पर उठा दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थानीय रीतियों के अनुसार, भूमि के प्रबन्धक को किराये पर देने का प्राधिकार रहता है। अतः तहसीलदार का कार्य भू-स्वामी पर बाध्यकारी था।
प्रश्न 15 अभिकर्ता कौन है? विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं को परिभाषित कीजिए। अभिकर्ता बनाम नौकर तथा अभिकर्ता बनाम न्यासी में अन्तर स्पष्ट कीजिए। अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण की आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिये।
Who is an Agent? Define various kinds of Agents. What is the difference between Agent vs. Servant and Agent vs. Trustee. What are the essentials of Agency by Ratification? Discuss.
उत्तर- अभिकर्ता (Agent) संविदा अधिनियम की धारा 182 अभिकर्ता (Agent) तथा स्वामी (Principal) की परिभाषा देती है। इस परिभाषा के अनुसार अभिकर्ता (Agent) वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों (third person) से संव्यवहारों (transactions) में किसी अन्य (जिसके द्वारा नियोजित है- स्वामी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित (Employed) है।
वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक या स्वामी (Principal) कहलाता है।
स्वाभी (Principal) तथा अभिकर्ता (Agent) के मध्य सम्बन्ध को अभिकरण कहते हैं। संक्षेप में अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक की ओर से कार्य करने हेतु या मालिक का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोजित होता है। अभिकर्ता अपने स्वामी की ओर से कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति तथा अपने स्वामी के मध्य संविदात्मक सम्बन्ध का सृजन कर मालिक को अन्य व्यक्ति के साथ मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से बाध्य कर सकता है। परन्तु मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से अभिकर्ता तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि इस विषय में उसकी स्वामी के साथ पृथक् संविदा न हो।
मुम्बई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मुम्बई बनाम आनरेबल मिनिस्टर फॉर मार्केटिंग, महाराष्ट्र स्टेट मंत्रालय, ए० आई० आर० 2015 बाम्बे 234 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिकरण की संविदा का निर्माण तभी होता है जब अभिकर्ता को तीसरे व्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अभिकर्ता कोई भी कार्य अपने लिए नहीं कर सकता।
अभिकर्ता होने के लिए संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक नहीं है। अतः एक अवयस्क अभिकर्ता हो सकता है। परन्तु एक अवयस्क व्यक्ति स्वामी (मालिक) नहीं हो सकता।
अभिकर्ता के प्रकार (Kinds of Agent) सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अभिकर्ता निम्न प्रकार के हो सकते हैं-
(1) सामान्य अभिकर्ता:
(2) विशिष्ट अभिकर्ता; तथा
(3) सार्वभौमिक अभिकर्ता।
सामान्य अभिकर्ता, वह अभिकर्ता है जो एक निश्चित सीमा या क्षेत्र के अन्तर्गत स्वामी की ओर से कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है। जबकि विशिष्ट अभिकर्ता उसे कहते हैं जो स्वामी द्वारा कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए नियोजित होता है जिसका उल्लेख उसके नियोजन के साथ किया गया हो। ऐसे अभिकर्ता द्वारा किये गये उस विशिष्ट कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया था। सार्वभौमिक अभिकर्ता वह अभिकर्ता है जो अपने स्वामी की ओर से वे सभी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है जो वैध तथा विधिसम्मत हो। सार्वभौमिक अभिकर्ता (Universal Agent) का अधिकार असीमित होता है।
व्यापार जगत द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं के प्रकार निम्न हैं-
(1) आढ़तिया (Factor);
(2) दलाल (Broker);
(3) प्रत्यापक अभिकर्ता (Del Credere Agent),
(4) नीलामकर्ता (Auctioner);
(5) उप अभिकर्ता (Sub-agent);
(6) सह-अभिकर्ता (Asst.-agent); तथा
(7) कमीशन एजेण्ट (Commission Agent) ।
(1) आढ़तिया (Factor) आढ़तिया एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बिक्री हेतु वस्तु या माल का कब्जा दे दिया जाता है। आढ़तिया एक ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता है जिसका कार्य साधारणतः स्वामी या मालिक के माल का विक्रय करना होता है जिसका कब्जा या नियन्त्रण स्वामी ने उसे दे दिया है।
(2) दलाल (Broker) दलाल भी एक प्रकार का व्यापारिक अभिकर्ता है। दलाल की नियुक्ति भी स्वामी की ओर से सम्पत्ति या माल के क्रय या विक्रय हेतु की जाती है। परन्तु आढ़तिया की भाँति दलाल को क्रय या विक्रय को वस्तु का नियन्त्रण या कब्जा नहीं दिया जाता।
(3) प्रत्यापक अभिकर्ता (Del Credere Agent)- यदि एक अभिकर्ता मालिक या स्वामी है, वह प्रत्याभूति (guarantee) दे कि जिस व्यक्ति के साथ वह मालिक की ओर से सम्बन्ध बनाने हेतु संविदा कर रहा है यदि वह अन्य व्यक्ति से संविदा भंग करेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा तो ऐसे अभिकर्ता को प्रत्यापक अभिकर्ता कहते हैं। ऐसी प्रत्याभूति (guarantee or surety) देने के लिए प्रत्यापक अभिकर्ता अधिक कमीशन माँगता है तथा इस कमीशन को प्रत्यापक कमीशन (Del credere commission) कहते हैं। प्रत्यापक अभिकर्ता का दायित्व चूँकि गौण (Secondary) होता है अतः प्रत्यापक अभिकर्ता का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब मूल संविदा भंगकर्ता (अन्य व्यक्ति) अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल हो जाता है।
(4) नीलामकर्ता (Auctioner) – यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामी या मालिक द्वारा किसी सम्पत्ति या वस्तु का विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा करने के लिए नियोजित होता है तो उसे नीलामकर्ता कहते हैं।
(5) उप अभिकर्ता (Sub-Agent) – ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अभिकर्ता द्वारा नियुक्त एवं उसके नियन्त्रण में कार्य करते हैं।
(6) सह अभिकर्ता (Assistant Agent) जब मालिक अपने कार्यों को करने के लिए दो से अधिक व्यक्तिों को एक ही साथ नियुक्त करता है तो वे पृथक् पृथक् या संयुक्तरूपेण उत्तरदायी होते हैं, उन्हें सह-अभिकर्ता कहा जाता है।
(7) कमीशन एजेण्ट (Commission Agent)- जो व्यक्ति मालिक की तरफ से वस्तुओं का क्रय-विक्रय यथासम्भव अच्छी शर्तों पर करता है तथा अपने कार्यों के बदले में कमीशन प्राप्त करता है उसे कमीशन एजेण्ट कहते हैं। वस्तुओं के क्रय के मामलों में यह मालिक से उतना ही मूल्य प्राप्त कर सकता है जितने पर कि उसने खरीदा है। इस कारण से कमीशन अभिकर्ता कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है कि उसने दोनों पक्षकारों के मध्य संविदा स्थापित किया है। [बनवारी लाल एण्ड कम्पनी बनाम सुन्दरम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, ए० आई० आर० (1979), एन० ओ० सी० 22 (मद्रास)]
अभिकर्ता बनाम नौकर में अन्तर (Difference between Agent v. Servant)- अभिकर्ता अपने मालिक का अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करने का माध्यम होता है या जो अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे व्यक्ति से संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है जबकि नौकर साधारण घरेलू कार्यों के लिए लगाये जाते हैं।
(1) अभिकर्ता को अपने मालिक का कार्य करने तथा तीसरे व्यक्ति के साथ उनका संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार होता है, जबकि नौकर को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
(2) मालिक अपने अभिकर्ता को कार्य करने का निर्देश देता है जबकि स्वामी द्वारा नौकर को कार्य करने और कार्य किये जाने के तरीके के सम्बन्ध में आदेश देता है।
(3) अभिकर्ता मालिक के आदेशानुसार कार्य तो करता है, परन्तु उसके नियन्त्रण में नहीं रहता है जबकि नौकर स्वामी के नियन्त्रण में रहते हुए उसके आदेशानुसार कार्य करता है।
(4) अभिकर्ता को पारिश्रमिक वेतन, कमीशन या दलाली के रूप में मिलता है जबकि नौकर को वेतन या मजदूरी मिलती है।
(5) अभिकर्ता कई मालिकों के लिए कार्य कर सकता है किन्तु नौकर केवल एक ही की नौकरी कर सकता है।
(6) मालिक अपने अभिकर्ता की दुष्कृतियों के लिए तभी दायी होगा जब उसने उसे अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर किया हो। जबकि स्वामी अपने नौकर द्वारा नौकरी के क्षेत्र में की गई दुष्कृतियों के लिए उत्तरदायी होता है।
अभिकर्ता बनाम न्यासी में अन्तर (Difference between Agent v. Trustee)- न्यासी वह व्यक्ति है जो दूसरे को सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों के हितार्थ अथवा कानून द्वारा अनुमति दिये गये या न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारित करता है-
(1) अभिकर्ता अभिकरण की विषय-वस्तु का अपने मालिक के लिए प्रतिनिधि मात्र होता है जबकि न्यासी न्यासवत् सम्पत्ति का विधिक स्वामी होता है।
(2) अभिकर्ता का सम्बन्ध सम्पत्ति से नहीं होता है उसका कुछ भी कार्य हो सकता है जबकि न्यास की विषयवस्तु सदैव सम्पदा होती है। जो धनराशि या चल-अचल किसी सम्पत्ति के रूप में हो सकती है।
(3) अभिकर्ता न तो अपने नाम से बाद प्रस्तुत कर सकता है और न तो उसके हॉ खिलाफ वाद प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि न्यासी अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके विरुद्ध बाद लाया भी जा सकता है अर्थात् यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है।
अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण का सूजन (Creation of Agency by Ratification)- संविदा विधि की धारा 196 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे अभिकर्ता के रूप में नियोजित नहीं किया गया है किसी व्यक्ति के लिए, परन्तु उस व्यक्ति की जानकारी तथा उस व्यक्ति के द्वारा अधिकार न दिये गये होने पर भी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जिसके लिए ऐसा किया गया है यह विकल्प प्राप्त है कि या तो वह उसकी जानकारी तथा प्राधिकार के अभाव में किये गये कार्य को स्वीकार करे (अनुसमर्थन दे) या उस कार्य को अस्वीकार कर दे। यदि वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया गया है उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है तो उस कार्य के परिणामों के लिए अनुसमर्थन करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अधिकृत था परन्तु यदि यह व्यक्ति उस कार्य का अनुसमर्थन नहीं करता है तो वह कार्य उस पर बाध्यकारी नहीं होगा।
उक्त अनुसमर्थन (Ratification) अभिव्यक्त हो सकता है या विवक्षित। अभिव्यक्त अनुसमर्थन स्पष्टतः मौखिक या लिखित रूप से किया जाता है जब कि विवक्षित अनुसमर्थर पक्षकार के आचरण के आधार पर अनुमानित किया जाता है। (धारा 197)
इस प्रकार स्वामी द्वारा अभिकर्ता के कार्य के अनुसमर्थन द्वारा भी अभिकरण का सूजन हो सकता है।
अनुसमर्थन द्वारा वैध अभिकरण हेतु आवश्यक शर्ते –
(1) प्रश्नगत कार्य अभिकर्ता ने अपनी ओर से न कर दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा दूसी व्यक्ति के निमित्त किया हो (धारा 196)। धारा 196 के अनुसार प्रश्नगत कार्य का अनुसमर्थन उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसकी ओर से या जिसके निमित्त कार्य किया गया हो।
(2) अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति का अस्तित्व (existence) होना चाहिए तथा वह व्यक्ति संविदा करने हेतु सक्षम (competent) होना चाहिए। यदि जिस व्यक्ति की ओर से तथा जिसके निमित्त प्रश्नगत कार्य किया गया है, वह अवयस्क है तो वह वयस्क होने पर अनुसमर्थन नहीं कर सकता। कार्य की तिथि को स्वामी का वयस्क होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि एक कम्पनी कार्य की तिथि को निगमित या पंजीकृत नहीं थी, अस्तित्व में नहीं मानी जा सकती, तथा वह अपने अस्तित्व या निगमन के पूर्व के कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकती।
(3) वैध अनुसमर्थन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि अनुसमर्थनकर्ता ने प्रश्नगत कार्य की प्रकृति की जानकारी के पश्चात् उसका अनुसमर्थन किया हो। धारा 198 के अनुसार वह व्यक्ति किसी कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकता, जिस प्रश्नगत कार्य के बारे में जानकारी न रही हो।
(4) धारा 199 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य का अनुसमर्थन करता है तो वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार (Whole Transaction) का अनुसमर्थन करता है जिसका अंश प्रश्गनत कार्य है।
(5) जिस कार्य का अनुसमर्थन किया जा रहा है वह कार्य उस अन्य व्यक्ति के लिए क्षतिकर नहीं होना चाहिए जिसके साथ किए गए संव्यवहार (कार्य) का अनुसमर्थन स्वामी को करना है। संविदा अधिनियम की धारा 200 के अनुसार अनुसमर्थन किया जाने वाला कार्य यदि ऐसा है कि वह कार्य यदि अभिकर्ता द्वारा अधिकार के साथ किया जाता है तो उस अन्य व्यक्ति (जिसके साथ कार्य किया गया है) को क्षति पहुँचाता या उसके किसी हित या अधिकार को समाप्त कर देता। इस प्रकार के कार्य का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता।