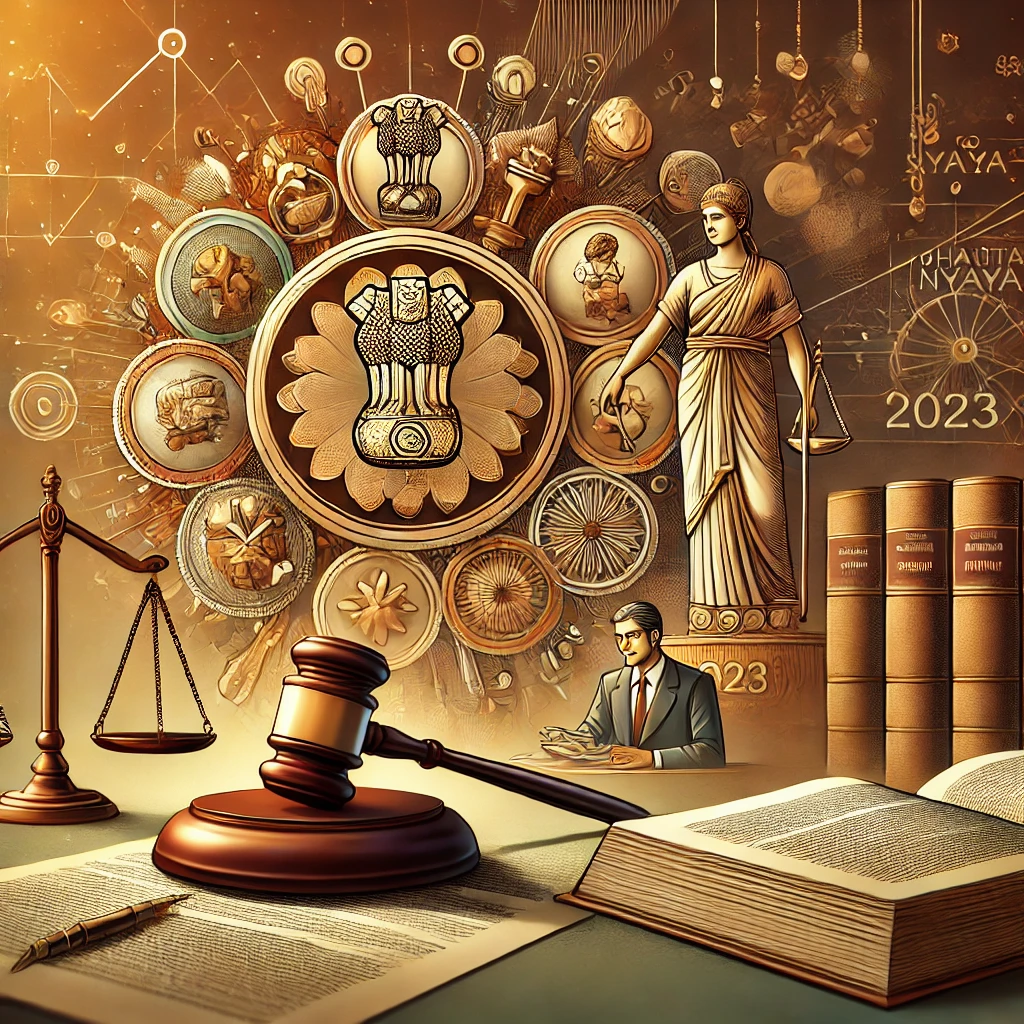-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
प्रश्न 1. (क) 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। Discuss the important features of the development of International law in 21st century.
(ख) ‘अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ की परिभाषा दीजिए तथा इसके ‘प्रकृति’ की विवेचना कीजिए। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में भिन्नता स्पष्ट करें। Define ‘International Law and discuss its nature. Distinguish between Public International Law and Private International Law.
उत्तर (क ) – अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिकल्पना इस विचार पर आधारित है कि सम्पूर्ण विश्व एक विशाल राष्ट्र है तथा विश्व के सभी राष्ट्र इस महान विश्व राष्ट्र की इकाइयाँ हैं। जिस प्रकार एक राष्ट्र अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा उनके मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करने के लिए विधि निर्मित करता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उद्देश्य भी स्वतन्त्र राष्ट्रों के मध्य उनके सम्बन्धों को नियन्त्रित करना है जिससे राष्ट्रों के बीच युद्ध या शोषण की सम्भावनाओं को यथासम्भव नियन्त्रित किया जा सके। यद्यपि लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की गई, द्वितीय विश्वयुद्ध ने इसकी असफलता को उजागर कर दिया। अब समय आ गया था कि विश्व के राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्त्रित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रयास किया जाय तथा इन्हीं प्रयासों का परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि संयुक्त राष्ट संघ घोषणा-पत्र के पूर्व रूढ़ियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के रूप में विद्यमान अवश्य थी परन्तु उसे निश्चित तथा आधुनिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र (Charter of U.N.O.) द्वारा प्रदान किया गया।
आज के विश्व में एक राष्ट्र भी समाज के आम व्यक्तियों पर परस्पर रूप से निर्भर हो गया है उसी प्रकार एक राष्ट्र की गतिविधियाँ दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि विश्व के राष्ट्र किसी एक सर्वमान्य विधि के अन्तर्गत अपने कार्यकलापों को नियन्त्रित रखें। यही अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख उद्देश्य है। ‘अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओपेनहाइम एवं जेरमी बेन्थम द्वारा सन् 1780 में किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विधि को कुछ प्रख्यात विधिशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्न हैं-
“राष्ट्रों की विधि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि परम्परागत तथा सन्धियों से उत्पन्न ऐसे नियम हैं जिन्हें कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा आपसी व्यवहार में वैध रूप से एक-दूसरे पर बाध्यकारी माना जाता है।” – ओपेनहाइम
”अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन सिद्धान्तों और नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राज्य परस्पर सम्बन्धों में अपने ऊपर बन्धनकारी मानते हैं और ये (नियम) सम्प्रभु राज्यों की सहमति पर आधारित होते हैं।” –हाम्स (Hughes)
“अन्तर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि उननियमों के निकाय (body of rules) का नाम है जो कि साधारण परिभाषा के अनुसार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में उनके ‘आचरण” को नियन्त्रित करते हैं।” – हेन्स केल्सन
“अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों का समूह है जिनका अधिकांश भाग उन आचरण के सिद्धान्तों तथा नियमों से बना हुआ है जिनको राज्य अपने सम्बन्धों में पालन करने के लिए अपने को बाध्य समझते हैं अतः वे उनका साधारणतया पालन करते हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
(अ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के संचालन सम्बन्धी विधि के नियम, उनके एक-दूसरे के प्रति तथा राज्यों और व्यक्तियों के प्रति सम्बन्ध; और
(ब) व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ विधि नियम जो कि ऐसे व्यक्तियों के अधिकार या कर्त्तव्य को निर्धारित करते हों जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सम्बन्धित प्रकरण हो।” स्टार्क
उपरोक्त कुछ विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई परिभाषाओं से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निम्न आवश्यक तत्व परिलक्षित होते हैं- (1) अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों को विधि है न कि राष्ट्र की विधि।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय विधि से राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध नियन्त्रित होते हैं।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्येक राष्ट्र अपने अन्य राष्ट्र के साथ परस्पर सम्बन्धों के विषय में अपने पर बाध्यकारी मानते हैं।
(1) अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों की विधि है— अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय स्वतन्त्र राष्ट्र हैं, यह विधि राष्ट्रों पर लागू होती है। यह तत्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि (National laws or Municipal law) से पृथक करता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों पर लागू होती है। एक आम सहमति के आधार पर विश्व शान्ति तथा विश्व समृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु तथा राष्ट्रों के मध्य आपसी सम्बन्धों को मधुर बनाने हेतु इस विषय में कुछ नियमों को एकत्र कर संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र का स्वरूप प्रदान किया गया। एक विश्व संगठन का निर्माण कर इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का दायित्व इस विश्व संगठन पर डाला गया। अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों की विधि होने के कारण राष्ट्रों के ऐसे क्रिया कलापों को नियन्त्रित करती है जो उनके आपसी सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय (Subjects) एक आम नागरिक न होकर स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। यह विधि प्रत्यक्षतः राष्ट्रों पर ही लागू होती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुपालन तथा इसके अन्तर्गत उपस्थित समस्याओं को निपटाने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई है।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय विधि से राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध नियन्त्रित होते हैं- अन्तर्राष्ट्रीय विधि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले नियम तथा उपनियम को अपने में समेटे हुए है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सम्प्रभुता का सम्मान करते हुए किन कार्यों को कर सकेगा या किस प्रकार के कार्यों को करना वर्जित है इसका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय विधि में मिलता है। इन नियमों को एक आम सहमति पर इस आधार पर स्वीकार किया गया है क्योंकि यह विश्व शान्ति तथा विश्व समृद्धि के लिए आवश्यक है।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अभाव में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मनमानापन व्यवहार तथा ऐसे कार्य कर सकते हैं जो विश्व शान्ति तथा राष्ट्रों के आपसी मधुर सम्बन्धों में बाधक हों।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्येक राष्ट्र अपने पर बाध्यकारी मानते हैं- अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यता का आधार (Pacta Sunt Sarvanda) पेक्टा सन्ट सर्वण्डा का सिद्धान्त है जिसका सरल अर्थ है सन्धियों का (सम्मान कर) अनुपालन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का जन्म सदस्य राष्ट्रों की आम सहमति के फलस्वरूप हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑफ नेशन्स अस्तित्व में था परन्तु इसकी विफलता ने तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका ने विश्व के समस्त राष्ट्रों को एक मंच पर आकर सहमति के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था करने को बाध्य किया जिससे कि विश्व में शान्ति तथा आपसी सौहार्द्र बढ़े। कुछ प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि के प्रयासों से एक आम सहमति के आधार पर नियमों के एक समूह को स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपने पर बाध्यकारी होने की घोषणा की इन नियमों में नवीन राष्ट्र सदस्यों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। इसी सहमति के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को राष्ट्र अपने पर बाध्यकारी मानते हैं।
परन्तु कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा उन्नति के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिकल्पना में परिवर्तन हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को आधुनिक परिभाषा (Modern definition) का जन्म हुआ।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा ओपेनहाइम ने सन् 1992 में अपनी पुस्तक ‘इण्टरनेशनल लॉ’ के नवें संस्करण में की इस परिभाषा में ओपेनहाइम ने सन् 1955 में अपनी उपर्युक्त पुस्तक के आठवें संस्करण में दी गई परिभाषा को काफी हद तक परिवर्तित किया तथा इस परिभाषा की आलोचना के परिप्रेक्ष्य में अपनी पूर्व की परम्परागत परिभाषा की खामियों को दूर किया।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ढाँचे में हुए प्रमुख परिवर्तन-पिछले कुछ दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ढाँचे में कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए जिसके फलस्वरूप परम्परागत परिभाषा को परिवर्तित करना आवश्यक हो गया। ये परिवर्तन निम्न हैं-
(1) पहले राज्य तथा सिर्फ राज्य को ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाता था परन्तु पिछले कुछ दशकों के दौरान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (Organizations) तथा संस्थानों का जन्म हुआ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत इन्हें भी कुछ अधिकार तथा कर्त्तव्य सौंपे गये। अतः अब अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संस्थानों को भी स्थान देना आवश्यक हो गया। अब अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा संस्थान भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय- वस्तु माने जाते हैं।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत परिभाषा में व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया था अब अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्ति को भी निश्चित अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किये गये। ऐसा विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् हुआ। अब अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आधुनिक परिभाषा में व्यक्ति को भी अन्तरर्राष्ट्रीय विधि की विषयवस्तु माना गया है।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत परिभाषा में बहुराष्ट्रीय निगमों को स्थान नहीं दिया गया था। आधुनिक युग में बहुराष्ट्रीय निगमों का जन्म हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकलाप को भी नियन्त्रित किया जाता है।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत परिभाषा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम सिर्फ रूढ़ियों तथा सन्धियों से ही बने हैं परन्तु यह सत्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कई नियम सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। परम्परागत परिभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस स्रोत की उपेक्षा की गई है।
(5) अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत परिभाषा में ‘नियमों के समूह’ शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम स्थायी प्रकृति के हैं तथा इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। परन्तु आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि गतिशील तथा जीवन्त विधि है। इसके नियम समय के अन्तराल के साथ अनुभवों तथा अनुबन्धों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आधुनिक परिभाषा – अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आधुनिक – परिभाषा ओपेनहाइम ने अपनी पुस्तक ‘इण्टरनेशनल लॉ के नौवें संस्करण में सन् 1992 में दी स्टार्क ने भी अपनी पुस्तक ‘इण्ट्रोडक्शन टु इण्टरनेशनल लॉ के दसवें संस्करण में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आधुनिक परिभाषा दी है।
ओपेनहाइम के अनुसार- अन्तर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में उन पर आबद्धकर है। ये नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के सम्बन्धों को शासित करते हैं किन्तु अकेले राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्त्तव्यों के विषय हो सकते हैं।”
यह परिभाषा परम्परागत परिभाषा से अधिक व्यापक है क्योंकि यह परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा व्यक्तियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय स्वीकार करती है।
स्टार्क ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि की आधुनिक परिभाषा दी है। स्टार्क के अनुसार – ” अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि का वह समूह है जिनका अधिकांश भाग आचरण के उन सिद्धान्तों तथा नियमों से बना है, जिनका अनुपालन करने के लिए राज्य अपने को बाध्य अनुभव करते हैं। अतः वे अपने पारस्परिक सम्बन्धों में इसका सामान्यतः अनुपालन करते हैं। तथा इनमें सम्मिलित हैं-
(क) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों की कार्यप्रणाली एवं उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा राज्यों एवं व्यक्तियों के सम्बन्धों के वैधानिक नियम तथा
(ख) कुछ वैधानिक नियम जो व्यक्तियों तथा गैर-राज्य इकाइयों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सम्बन्धित हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति (Nature of International Law) – अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि कहा जा सकता है। क्या यह उसी तरह की विधि है जैसी कि राष्ट्रीय विधि इस विषय पर 1 विधिशास्त्रियों के विचारों में काफी भिन्नता रही है। यद्यपि राज्यों के सम्बन्धों को विनियमित करने वाले नियमों को पिछले लगभग 200 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता रहा है, फिर भी कई विधिशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते हैं। इसे केवल नैतिक बल (Moral Force) के आचरण की संहिता कहते हैं। दूसरा मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है तथा इसे उसी प्रकार विधि के रूप में माना जाता है, जैसे राज्यों की विधि को, जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है।
मनुष्यों का समाज तथा राज्यों का समाज अपने भिन्न स्वरूप तथा अपने वास्तविक आधार के कारण एक-दूसरे से समता करने योग्य नहीं है तथा व्यक्तियों के सम्बन्धों तथा राज्यों के सम्बन्धों को विनियमित करने वाली विधि की बाध्यकारी प्रकृति में भी अन्तर है। लेकिन जब से अन्तर्राष्ट्रीय समाज के अस्तित्व के पक्ष में तर्क दिया जाने लगा है, तब से यह कहा जाने लगा कि कम से कम इसका अस्तित्व राज्यों के कतिपय आचरणों को विनियमित करता है। आधुनिक समय में विश्व को वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय माना जाता है। राज्यों के लिए जो विश्व समुदाय के सदस्य हैं, रूढ़ियों तथा सन्धियों के द्वारा नियमों को बनाया गया है। राज्य इन नियमों को मान्यता देते हैं तथा इनका पालन करते हैं और इस बात का विश्वास करते हैं कि उनके आचरणों को विनियमित करने के लिए नियमों का समूह अस्तित्व में है। ये नियम राज्यों द्वारा विदेशी कार्यालयों, राष्ट्रीय न्यायालयों तथा अन्य सरकारी अंगों के माध्यम से प्रयोग में लाये जाते हैं। राज्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से विधिक रूप से बाध्य हैं।
सार्वजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में भिन्नता- सार्वजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में निम्नलिखित उल्लेखनीय भिन्नतायें हैं-
(1) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों तथा कुछ अंशों तक व्यक्तियों से सम्बन्धित है, जबकि वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतया दो राज्यों के व्यक्तियों से सम्बन्धित है।
(2) वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का अंग है, जबकि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि ऐसी नहीं है।
(3) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों में समान रूप से लागू की जाती है, जबकि वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती है।
(4) वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतया विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधान द्वारा लागू की जाती है, जबकि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि रूढ़ियों तथा सन्धियों द्वारा विकसित होती है।
(5) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि सभी राज्यों पर लागू होती है। अतः इस विधि का एक मुख्य लक्षण है सार्वभौमिकरण ( Universalization) । अन्तर्राष्ट्रीय विधि सभी राज्यों की सभी गतिविधियों से सम्बन्धित होती है चाहे वह अन्तरिक्ष में हो या चन्द्रमा या अन्य आकाश पिण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यह विशेषता इसको वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से भिन्न करती है।
उत्तर (ख ) – आधुनिक युग में विधिशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों की सम्मति अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम रूढ़ि तथा सन्धियों से ही बने हैं। फिर भी तर्क तथा न्याय को भी उन मामलों में मान्यता देते थे, जहाँ राज्यों के अभ्यास उपलब्ध नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों तथा अधिकरणों ने अपने विनिश्चयों में इन कारकों को मान्यता दी। अतएव वर्तमान शताब्दी में प्रोशियस शाखा का पुनरुत्थान हुआ। साधारणतया अब इसे माना जाने लगा है कि राज्यों के अभ्यास पर आधारित विधि के नियमों के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को न्याय के नियमों (Rules of Jusitce) से तथा विधि के सामान्य सिद्धान्तों से उपयुक्त रूप से अनुपूरित किया जा सकता है। इन नियमों को प्रोशियस द्वारा प्रयुक्त अर्थ में प्राकृतिक विधि या परिवर्तनीय सन्दर्भ सहित आधुनिक प्राकृतिक विधि के रूप में या अन्तर्राष्ट्रीय विधि की “प्रारम्भिक परिकल्पना” के रूप में या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के रूप में राज्यों की सामाजिक प्रकृति की मूल कल्पना के रूप में या संक्षेप में, तर्क से उद्भूत रूप में परिभाषित किया जाय। गोशियस शाखा वर्तमान विधिक स्थिति के काफी निकट है।
21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास जिन कारणों से हुआ, उसमें निम्नलिखित मुख्य है-
(1) पहली बार सार्वभौमिक प्रकृति के संगठनों की स्थापना की गयी। राष्ट्र संघ (League of Nations) (1919) तथा तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ (1945) प्रमुख रूप से विश्व शान्ति को बनाये रखने के लिए स्थापित किये गये।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पुनः अभूतपूर्व घटना है। स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (1921) तथा तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (1946) द्वारा राज्यों के कई विवादों को निपटाया गया।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा राज्यों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं को निपटाना वर्तमान शताब्दी का महत्वपूर्ण प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के विशिष्ट अभिकरण (Specialised Agencies) तथा क्रियाशील अभिकरण (Functional Agencies) मानव की बहुमुखी दशा को सुधारने का प्रयास करने के लिए स्थापित किये गये हैं।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम ऐसे कई विषयों पर बहुपक्षीय सन्धियों के निर्माण द्वारा बनाये गये हैं, जिनकी पूर्व शताब्दी में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में, अन्तरिक्ष, चन्द्रमा तथा खुला समुद्र (High Seas) बहुपक्षीय सन्धियों द्वारा शासित होते हैं।
(5) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण बीसवीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का महत्वपूर्ण अंग हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो अब तक संदिग्ध तथा अनिश्चित थे, क्रमबद्ध रूप से लिखित रूप में किये जा रहे हैं, जो सभी राज्यों पर या अधिकतर राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं।
(6) अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं रह गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा व्यक्तियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाने लगा है। व्यक्तियों को कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के समक्ष याचिकाओं को दाखिल करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।
इन सभी कारणों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उस स्थिति में पहुँचा दिया है, जिसको इसकी उत्पत्ति के समय सोचा भी नहीं गया था। नये-नये नियमों को नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के पास विधायन तथा न्यायालय है, जिनके विनिश्चयों को पक्षकारों पर बाध्यकारी माना जाता है। जो राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध अनुशास्ति (Sanction) लागू की जा सकती है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अपने सीमित प्रभाव के कारण अब भी निर्बल विधि है। किन्तु यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में इसका विकास इस तरह होगा जिससे यह सुदृढ़ तथा प्रभावी हो जाये। विधि की प्रभावी प्रणाली न केवल राज्यों द्वारा नियमों के उल्लंघन को कम करने में सहायता देगी बल्कि यह राज्यों को शान्तिपूर्वक रहने के लिए भी समर्थ बनायेगी।
प्रश्न 2. अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार क्या है? क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में एक विधि है? What is the basis of International Law. Is International Law a Law in true sense of them?
उत्तर- अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार (Basis of International Law)- वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना गया है। राज्य अपने | अभ्यास में इसके नियमों का पालन करते हैं। प्रश्न उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार क्या है अर्थात् इस विधि के नियम किन बातों पर आधारित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार | के सम्बन्ध में दो प्रमुख सिद्धान्त प्रचलित हैं-
(1) प्रकृतिवादी (Naturalists) सिद्धान्त तथा
(2) सार्थकतावादी (Positivists) सिद्धान्त।
(1) प्रकृतिवादी सिद्धान्त (Naturalists Theory) – प्रकृतिवादी सिद्धान्त के समर्थक ग्रोशियस (Gpotious), प्यूफेनडॉर्फ (Pufendorf) तथा वाट्टेल (Vattel) हैं। इन विधिशास्त्रियों का लेखन धर्मपरक विद्वानों जैसे सेन्ट आगस्टाइन (St. Augustine), विटोरिया (Vitoria) तथा सुआरेज (Suarez) के कार्यों द्वारा अत्यधिक प्रभावित था। ये विधिवेत्ता तर्क देते हैं कि सभी विधियाँ ईश्वर से प्राप्त होती हैं तथा वे ईश्वर की सर्वोच्च विधि को देवी विधि (Divine Law) मानते है इसलिए इसे प्राकृतिक विधि की अपेक्षा देवी विधि कहना अधिक उचित है।
उन्नीसवीं शताब्दी के लेखकों द्वारा इस मत की कड़ी आलोचा इस आधार पर की गयी है। कि यह मत अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि सही मायने में प्राकृतिक विधि का अर्थ सुनिश्चित नहीं है। अलग-अलग विधिशास्त्रियों द्वारा इसका अलग-अलग अर्थ दिया गया है। जैसे तर्क, न्याय या नैतिकता । अतः इस मत की आलोचना कई कारणों से की जा सकती है। प्रथम, प्राकृतिक विधि के नियमों का निश्चित रूप से निरूपण करना आसान नहीं है। इसकी अनिश्चितता के कारण यह कहना मुश्किल है कि कौन से प्राकृतिक विधि के नियम अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम हो सकते हैं। यह एक ऐसा विस्मयकारी दृष्टिकोण है, जिसे यदि प्रभावी किया जाता है तो इसके परिणाम केवल विस्मयकारी ही होंगे। दूसरा प्राकृतिक विधि के नियम स्थिर व अपरिवर्तनशील होते हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम समय व परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। तीसरा, प्राकृतिक विधि के अर्थ के सम्बन्ध में भी लेखकों का अलग-अलग मत है। जहाँ कुछ लेखक इसको दैवी विधान की संज्ञा देते हैं, वहीं कुछ लेखक इसको न्याय, विवेक तथा तर्क समझते हैं।
(2) सार्थकतावादी सिद्धान्त (Positivists Theory) – सार्थकतावादी सिद्धान्त के विधिशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्य की पारस्परिक सम्मति (Consent) पर आधारित है। जिन नियमों में राज्य की सम्मति प्राप्त नहीं होती है, वे नियम उस राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं। विधिशास्त्री बाईकरशोक (Bynkershock) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय | विधि का आधार राज्यों की सम्मति है। राज्यों की सम्मति किसी भी नियम का पालन करने के लिए दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, पहला अभिव्यक्त सम्मति (Express Consent) द्वारा तथा दूसरा विवक्षित सम्मति (Implied Consent ) द्वारा। अभिव्यक्त सम्मति सन्धियाँ करके या सरकारों के ज्ञापित समागम द्वारा दी जाती हैं जबकि विवक्षित सम्मति स्थापित प्रथा, अर्थात् रूढ़ि का पालन कर दी जा सकती है। इस प्रकार रूढ़ि तथा सन्धियाँ जिसके द्वारा राज्य की सम्मति प्राप्त की जाती है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार हैं। जब तक कोई राज्य विशेष अन्तर्राष्ट्रीय विधि के किसी विशिष्ट नियम को अपनी सम्मति नहीं देता, तब तक उस राज्य पर वह नियम बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। मार्टिन्स (Martens) तथा एन्जीलोट्टी (Anzilotti) भी इस बात के समर्थक हैं।
सम्मति सिद्धान्त की आलोचना कई लेखकों द्वारा विभिन्न आधारों पर की गई है। पहला अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सभी नियम, रूड़ियों तथा सन्धियों से ही नहीं बने हैं। उनमें से कुछ सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धान्तों से भी बनाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्टेटयूट के अनुच्छेद 38 (1) के अन्तर्गत इसे निश्चित रूप से मान्यता प्रदान की गयी है। दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कुछ नियम किसी राज्य की सम्मति के बिना ही उसके ऊपर बाध्यकारी होते हैं। सन्धि विधि पर वियना कन्वेंशन (Vienna Convention on the law of treaties) के अनुच्छेद 36 के अनुसार एक सन्धि किसी तीसरे राज्य पर भी बिना उसकी सम्मति के लागू हो सकती है। तीसरा, कुछ मामलों में राज्य अपनी इच्छा के विपरीत भी सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा बँधे रहते हैं। नये स्थापित राज्य, जो किसी भी नियम में अपनी सम्मति आरम्भ में नहीं देते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन आलोचनाओं से यह प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार के सम्बन्ध में न तो प्रकृतिवादी सिद्धान्त और न ही सम्मति का सिद्धान्त सत्य है।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार के सम्बन्ध में उपर्युक्त दो मतों में कौन सा मत उचित है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कोई मत अकेले अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि दोनों ही सिद्धान्तों से प्रभावित है। इसी कारण धार्मिक शाखा (Eclectic School) के विधिशास्त्रियों ने सार्थकतावादी (Positivist) तथा प्रकृतिवादी (Naturalist) शाखा के बीच के मार्ग को अपनाया है। धर्मवादी जैसे वाट्टेल (Vattel) विधि के दो वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं एक प्रकृतिवादी स्तर पर तथा दूसरा सार्थकतावादी स्तर पर।
इस तरह, उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्राकृतिक विधि तथा सम्मति से बनायी गयी विधि, दोनों पर ही आधारित है।
इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि पूर्णतया न तो. प्राकृतिक विधि पर और न ही राज्यों की सम्मति पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों में अधिकतर नियम राज्यों की सम्मति के आधार पर आधारित हैं, जबकि उनमें से कुछ वास्तव में प्राकृतिक विधि से बने हैं।
क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि है – चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्रों के सम्बन्धों तथा क्रिया-कलापों को नियन्त्रित करने के नियमों का समूह है अतः इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई स्वतन्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि को मानने से इन्कार कर दे तो उसके विरुद्ध क्या उपाय हैं। दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को बाध्यकारी मानने से इंकार करने वाले सम्प्रभु तथा स्वतन्त्र राष्ट्र के विरुद्ध कोई बाध्यकारी उपाय इस विधि में न होने के कारण यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में या यथार्थ में विधि है। इसकी बाध्यता शक्ति क्या है। आस्टिन ने यह कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि नहीं है बल्कि यह आचरण सम्बन्धी नियमों की संहिता है जिसे केवल नैतिकता का ही बल (force) प्राप्त है तथा इसमें अपने से वरिष्ठ की आज्ञा (command of sovereign) के समान बाध्यकारी बल (binding force) की कमी है। हॉल्स तथा चुफेन डार्फ ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वाटेल ने यहाँ तक कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि मूल में कुछ नहीं वरन् प्रकृति के नियम हैं जो राष्ट्रों पर लगाये गये हैं। हालैण्ड के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से इस बात में भिन्न है कि इससे राज्य की प्राधिकारपूर्ण शक्ति (Sovereign power of State) का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लोपकारी बिन्दु (Vanishing point of jurisprudence) है ।
उपरोक्त विचारों के प्रतिकूल हाल तथा लारेंस जैसे विद्वानों का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि न सिर्फ विधि के समान प्रवर्तनकारी है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से अपने नियमों तथा अनुशास्ति (Sanctions) दोनों रूपों में स्पष्टतया पूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बारे में यह आपत्ति की जाती है कि इस विषय के सम्बन्ध में सम्मान की भावना अति न्यून है तथा अनुशास्ति (Sanction or Punishment) की कोई प्रभावशाली प्रणाली नहीं है जिसे कानून तोड़ने वालों पर लागू किया जा सके और ऐसे बन्धनकारी उपायों के अभाव में इस विधि में पालन करने की प्रवृत्ति नहीं रह गयी है। इस तर्क के उत्तर में यह कहा गया है कि कानून की प्रवर्तनशीलता का विचार करते समय अनुशास्तियों (Sanctions of Punishment) को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ अनुशास्तियाँ ही प्रमुख कारण नहीं हैं जिनकी वजह से किसी वैध प्रणाली में कानून का पालन किया जाता है। उदाहरण के रूप में (राष्ट्रीय विधि) भारतीय दण्ड संहिता में हत्या के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान (Provision) है। फिर भी भारतीय समाज में प्रतिदिन कई हत्याएँ होती रहती हैं। यदि अनुशास्ति (Sanction of Punishment) ही विधि को बाध्यकारी बनाती तो संसार से हत्या का अपराध समाप्त हो गया होता।
केल्सन ने भी कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में देशज विधि (राष्ट्रीय विधि) पर आधारित कोई आदिम प्रकार की अनुशास्ति की प्रणाली नहीं अपनाई जाती और यही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अपनी मौलिकता) विशेषता है क्योंकि यह विधि स्वयं आधुनिकतम नवीन राजनीतिक परिभाषाओं की देन है जिसमें केवल बल (Force) को ही प्रवर्तन (enforcement) का एक मात्र कारण नहीं माना गया है।
ऑस्टिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यथार्थ में विधि न मानकर सिर्फ सकारात्मक नैतिकता माना है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक निश्चयात्मक विधि एक सम्प्रभु द्वारा अपने अधीनस्थ राज्य के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि समान सम्मति (सहमति) के आधार पर निर्धारित विधि है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अधिरोपित कर्त्तव्य नैतिक शक्ति द्वारा लागू किये जाते हैं अन्तर्राष्ट्रीय विधि जिनके ऊपर लागू होती है वे सम्प्रभु राष्ट्र हैं जिनके ऊपर कोई सम्प्रभुता (Sovereignty) नहीं है। ऑस्टिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता कहा है जिसमें सामान्य रूप से मान्य सम्मतियाँ सम्मिलित हैं।
स्टार्क ने ऑस्टिन के इस विचार का विरोध करते हुए निम्न आधार बताये-
(1) कई समुदायों में कुछ प्रथाओं तथा रूढ़ियों के पीछे कोई प्राधिकारिक वैध शक्ति (authorised legal power) नहीं होती परन्तु उनकी वैधता में इस आधार पर कोई अन्तर नहीं पड़ता।
(2) ऑस्टिन के विचार उनके अपने समय में भले ही ठीक रहे हों परन्तु उन्हें आज की परिस्थितियों में लागू नहीं माना जा सकता जहाँ सम्प्रभु (Sovereign) को भी विधि के शासन (rule of law) के अन्तर्गत लाया गया है।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को इसलिए यथार्थ में विधि नहीं माना है कि वह एक सम्प्रभु का अपने अधीनस्थ लोगों पर आदेश नहीं है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव सम्प्रभु के आदेश का स्वरूप धारण कर लेता है और उस राष्ट्र पर बाध्यकारी हो जाता है जिसके विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित किया जाता है। जहाँ तक अनुशास्ति (Sanction of Punishment) का प्रश्न है, इराक द्वारा कुवैत पर मनमाना आक्रमण कर कुवैत पर कब्जा करने के प्रकरण में हमने देखा कि इराक को जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मत का सम्मान करने से इंकार कर दिया था, किस प्रकार घुटने टेकने को बाध्य किया गया और वह भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि अब सकारात्मक नैतिकता न होकर प्रभावशाली विधि हो गई है।
प्रश्न 3. (i) “अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिन्दु है।” विवेचना कीजिए। “International Law is the vanishing point of Jurisprudence.” Discuss.
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। Write a short note on the subject of International Law,
उत्तर- अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधिशास्त्र का लुप्त प्राय बिन्दु है (International Law is the vanising point of Jurisprudence ) — विधिशास्त्री हॉलैण्ड (Holland) ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिन्दु (Vanishing Point) कहा है। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधिशास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि और विधिशास्त्र परस्पर समानान्तर हैं और इसी कारण दोनों ही एक-दूसरे से विशिष्ट एवं पृथक् हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही लुप्तप्राय बिन्दु पर एक ही हैं किन्तु वास्तव में दोनों पृथक हैं। उनके कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि न तो ये किसी प्रभुता सम्पन अधिकारी द्वारा निर्मित किये जाते हैं और न ही इनके नियमों का उल्लंघन करने पर कोई अनुशास्ति है। उनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि को केवल सौजन्यतावश (Courtesy) ही विधि की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन नियमों को विधि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालैण्ड के कथन को वर्तमान समय में, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुके हैं, उचित नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विधान, न्यायालय, अनुशास्ति, प्राधिकारी तथा प्रवर्तन तत्त्र का होना ही एक महत्वपूर्ण विकास है। इन सभी पहलुओं को देखने से प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि और विधिशास्त्र एक-दूसरे से पृथक नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र की ही एक शाखा है। वर्तमान समय में राज्यों के अभ्यास से यह प्रमाणित हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सच्चे मायने में विधि है।
उत्तर (ii)- अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय (Subjects of International Law) – अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति उन इकाइयों को कहा जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को धारण करते हैं। ओपेनहाइम के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति वह है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि में विधिक व्यक्तित्व धारण करता है अर्थात् वह जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इस प्रकार विषय है कि वह स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा शक्तियों का उपयोग कर सके और या तो प्रत्यक्षतः या अन्य राज्य के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता धारण करता हो अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्य सभी अधिकारों तथा कर्तव्यों को धारण करना किसी इकाई के लिए आवश्यक नहीं है। यदि कोई इकाई केवल कुछ कार्यों या केवल एक ही कार्य का अनुपालन करने में सक्षम है, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों द्वारा प्रावधान किया गया है, तो उस इकाई को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय होने के लिए क्षमता धारण करने वाला माना जायेगा। यह कहना अनुचित होगा कि सीमित क्षमता धारण करने वाली इकाइयों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई व्यक्तित्व नहीं है क्योंकि इनमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्य सम्पूर्ण अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के अनुपालन की क्षमता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि गतिशील होने के कारण वर्तमान समय में कुछ ऐसी इकाइयों को भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व धारण करने वाला मानती है, जो किसी समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व धारण नहीं करती थी। भविष्य में कुछ अन्य इकाइयों को भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त हो सकता है, यदि वे उस क्षमता को अर्जित कर लेती हैं, जिसे वे वर्तमान में धारण नहीं करती हैं।
विभिशास्त्रियों में इस बात पर मतभेद है कि किस इकाई को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाय। इस मतभेद के कारण तीन प्रमुख मतों की उत्पत्ति हुई है, जो निम्नलिखित हैं –
(1) यथार्थवादी सिद्धान्त (Realist Theory)- इस मत में “केवल राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं।” यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत अवधारणा है, जिसमें केवल प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाता था। इस सिद्धान्त के अनुसार केवल राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अधिकारों तथा बाध्यताओं के धारक होते हैं। इस सिद्धान्त को यथार्थवादी सिद्धान्त कहा जाता है।
(2) कल्पित सिद्धान्त (Fictional Theory)—यह सिद्धान्त यथार्थवादी सिद्धान्त के विपरीत है। इस सिद्धान्त के अनुसार केवल व्यक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों के पास अपनी इच्छा को प्रकट करने की क्षमता नहीं है, राज्य व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करने वाली अमूर्त संरचना हैं। केल्सन के अनुसार राष्ट्रीय विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उद्देश्य मानव के लिए है। राष्ट्रीय विधि प्रत्यक्ष रूप से उन पर बाध्यकारी होती है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात् राज्यों के माध्यम से, बाध्यकारी होती है। यह सिद्धान्त इस परिकल्पना पर आधारित है कि राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य उन व्यक्तियों के अधिकार तथा कर्तव्य होते हैं जिनसे वह गठित होता है तथा इसलिए अन्ततोगत्वा व्यक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। इस सिद्धान्त को कल्पित सिद्धान्त कहने का आशय यही है कि इसके अनुसार राज्य को कल्पना मात्र माना गया है।
(3) क्रियात्मक सिद्धान्त (Functional Theory) – उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों का वर्तमान समय में विश्लेषण किया जाय, तो दोनों ही सिद्धान्त सही नहीं होंगे। यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अधिकतम अधिकारों तथा कर्तव्यों को राज्य के प्रति निर्दिष्ट करना है लेकिन पूर्व के 50 वर्षों में इसमें मूलभूत परिवर्तन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बड़ी मात्रा में अन्य नयी इकाइयों का सम्मेलन हुआ है। राज्यों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा व्यक्तियों को अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कई विधिक कार्य करते हैं तथा उनका विधिक व्यक्तित्व भिन्न होता है। यही व्यक्तियों के साथ भी है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कुछ अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किये गये हैं। यदि वे अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं; तो इसके लिए दण्ड का प्रावधान भी है। पुनः कुछ मामलों में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा दिये गये अधिकारों का दावा करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।
अतः स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों की स्थिति समयानुसार काफी परिवर्तित हो गयी है। मूल रूप से प्रभुत्वसम्पन्न राज्य अनतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक मात्र कर्ता थे। किन्तु वर्तमान समय में, नई गैर राज्य इकाइयों, जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संस्थानों और व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधिक विषयों की प्रास्थिति (Status) तथा श्रेणी प्रदान की गयी है।
प्रश्न 4. (i) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विधिमान्य स्रोत कौन-कौन से हैं? उनके सापेक्षित महत्व का विवेचन करें। What are the recognized sources of International Law? Explain their relative importance?
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सन्धियों के महत्व की विवेचना करें। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उत्तरोत्तर विकास में सन्धियों की भूमिका पर प्रकाश डालें। Discuss the importance of treaties as a source of International Law. Throw light on the role of treaties on successive development of International Law.
उत्तर (i) – किसी विधि के स्रोत उन सामग्रियों को माना जा सकता है जिनसे उस विधि का उद्भव होना माना जाता है। स्टार्क के अनुसार – अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में उन सामग्रियों को परिभाषित किया जा सकता है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता दी हुई परिस्थितियों में (विद्यमान परिस्थितियों में) लागू होने वाले नियमों का विनिश्चयन करते हैं।”
स्त्रोत शब्द से तात्पर्य उस विधि (तरीका Method) तथा प्रक्रिया से है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का जन्म हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के औपचारिक तथा सारवान् दो प्रमुख स्रोत हैं। औपचारिक स्रोत वे स्रोत हैं जो विधिक प्रक्रिया तथा विधि (Method) के तौर पर नियमों का सृजन करते हैं जो सामान्य रूप से किसी पर लागू होती है। सारवान् स्रोत वे हैं जो नियमों के अस्तित्व का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं यदि ये साबित कर दिये जायें तो बाध्यकारी हो जाते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्न चार प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया है-
(1) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (Convention) या सन्धिय
(2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएँ:
(3) सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य विधि सिद्धान्त;
(4) न्यायिक निर्णय; तथा
(5) सबसे योग्य विद्वानों द्वारा भाष्य टीकाएँ तथा उपदेश
(1) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सन्धियाँ (International Conventions or International Treaties) – सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के पक्षकार सन्धि द्वारा संविदा करके कोई संगठन बना सकते हैं तथा अपने को उस संगठन द्वारा पारित प्रभाव से बाधित करने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। सन्धियों के प्रमुख दो प्रकार होते हैं-
(a) विधि विषयक सन्धियाँ- ये सन्धियाँ ऐसे सामान्य नियम निश्चित करती हैं जो राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं और राज्यों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए या उनके भावी अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के लिए नये सामान्य नियम घोषित करती हैं।
(b) वे सन्धियाँ जो सन्धि या संविदा करने वाले राज्यों के बीच किसी विशेष मामले का निपटारा करती हैं जैसे पेरिस घोषणा (1856), जिनेवा कन्वेन्शन्स, 1864, 1906, 1929, संयुक्त राष्ट्र संघ का शासनपत्र (Charter) 1943, जिनेवा समुद्र सन्धि, 1958 तथा वियना कन्वेन्शन, 1961 आदि ।
(2) अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ (International Customs) – प्रथाएं या रूढ़ियाँ विधि की प्राचीन तथा मौलिक स्रोत हैं। रूढ़ियाँ इस प्रकार के नियम के समान हैं जो कि एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक क्रम के उपरान्त विकसित हुए तथा जिनको स्वीकार कर अन्तर्राष्ट्रीय समाज में विधि का स्थान दिया गया। आधुनिक युग में प्रथाओं को स्रोत के रूप में एक प्रमुख स्त्रोत माना गया है।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियम के अनुच्छेद 38 (ख) ने अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि को स्वीकृत विधियों के सामान्य व्यवहार के साक्ष्य के रूप में मान्यता दी है। रूढ़ि तथा प्रथा शब्द अक्सर पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं। परन्तु उनमें अन्तर है। प्रथा (usage) वास्तव में रूढ़ि (custom) की प्रारम्भिक अवस्था है। प्रथा (usage) वे आदतें (habits) या व्यवहार हैं जो राज्यों द्वारा बार-बार व्यवहार लें लाये गये हैं। स्टार्क के अनुसार- “जहाँ रूढ़ि (Custom) प्रारम्भ होती है वहीं प्रथाएं समाप्त होती हैं” अर्थात् प्रथाएँ रूढ़ियों में विलय हो जाती हैं। प्रथा वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार हैं जिसे अभी विधि (law) का बल प्राप्त नहीं हो पाया है। प्रथाएं आपस में परस्पर विरोधी हो सकती हैं परन्तु रूढ़ियों (custom) के साथ ऐसा नहीं है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि रूढ़ि (custom) में पूर्व प्रथा (usage) का अस्तित्व होता हो कुछ मामलों में प्रथाएँ (usage) रूदियाँ (custom) बन जाती हैं. कुछ में नहीं कभी-कभी सन्धियों से भी रूढ़ियों (custom) का जन्म होता है।
(3) विधि के सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Law) – अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि (statute) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम को भी लागू करने का प्रावधान करती है।
अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थानीय न्यायालय ने चोरजोब फैक्ट्री (Chorzov Factory ) 1927 के सम्बन्ध में व विधि के सामान्य सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए प्राङ्गन्याय (Res judicata) और म्यूज के जल से मार्गान्तरीकरण 1937 के प्रकरण में विबन्ध (estoppel ) का प्रयोग किया था।
(4) न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) – अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि विधान (Statute) के अनुच्छेद 38 में यह निर्देश दिया गया है कि विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक साधन के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं अन्तर्राष्ट्रीय संविधि (Statute) के अनुच्छेद 59 में न्यायालय के निर्णय पक्षकारों तथा उपविशिष्ट विषय को छोड़कर अन्यत्र बाध्य नहीं है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम स्थायी न्यायालय तथा उसके उत्तराधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय दोनों में संसार की मुख्य विधायी पद्धतियों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों की उच्च कोटि की ख्याति एवं निष्पक्षता की दृष्टि से उनके निणयों को न्यायिक पूर्ण दृष्टान्त के वास्तविक गुणों से युक्त माना गया है।
(5) अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थों के रचनाकार (Text writers) – विधिवेत्ताओं के कार्य (Acts of Jurist) तथा टीकाकारों की टीकाएँ- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि (Statute) के अनुच्छेद 38 न्यायालय को विधि के नियम निर्धारित करने के लिए इस विषय पर भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सर्वोत्कृष्ट योग्यता रखने वाले प्रवीण लेखकों की शिक्षाओं को सहायक साधन के रूप में लागू करने को प्राधिकृत करता है। पहली बात तो यह है कि लेखकों की कृतियों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात यह है कि लेखकों की रचनाएँ स्वतन्त्र रूप से विधि के लिए स्रोत नहीं हैं, उनके द्वारा ऐसे साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किये जाते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि विधि का स्वरूप क्या होना चाहिए।
विधि का यह अन्तिम स्रोत गौड़ स्रोत माना जाता है। परन्तु प्रथम चार स्रोत विधिमान्य एवं प्रमुख स्रोत माने जाते हैं।
उत्तर (ii)- सन्धि (treaty) या अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शनों को आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियम के अनुच्छेद 38 (1) (क) के अन्तर्गत सामान्यतया विशिष्ट कन्वेंशन्स या सन्धियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथम स्त्रोत के रूप में मान्यता दी गई है।
सन्धियों की विधि (law of treaties) पर 1969 में आयोजित वियेना कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 ने सन्धि की परिभाषा दी है। इसके अनुसार सन्धि एक ऐसा करार है जिसमें दो या दो से अधिक राज्य (राष्ट्र) आपस में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा शासित हों। परन्तु यह परिभाषा संकीर्ण है। प्रोफेसर श्वार्जन वर्गर द्वारा दी गई सन्धि की परिभाषा के अनुसार सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों (subjects) या राज्यों के मध्य करार हैं जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न होते हैं ।
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों दो प्रकार की होती हैं –
(1) विधि का निर्माण करने वाली सन्धियों; तथा
(2) संविदात्मक सन्धियाँ ।
(1) विधि का निर्माण करने वाली सन्धियाँ (Law Making Treaties)— विधि का निर्माण करने वाली सन्धियों के प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के पश्चात् विधि निर्माण करने वाली सन्धियों के विकास को गति मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि रूड़ियाँ, जिन्हें अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य स्रोत माना जाता था, अपर्याप्त साबित हुई। परिणामस्वरूप राष्ट्रों (राज्यों) ने यह आवश्यक समझा कि सन्धियों की जाएँ जिससे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने सम्बन्ध स्थापित किये जायें। विधि निर्माण करने वाली सन्धियों को पुनः दो भागों में बाँट सकते हैं-
(1) ऐसी सन्धियाँ जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक नियमों की घोषणा की गयी हो— संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र इस प्रकार की सन्धियों का – सर्वोत्तम उदाहरण है।
(2) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ जिनमें सामान्य सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया हो – ये सन्धियाँ अधिकतर राष्ट्रों द्वारा की गई हैं। इस प्रकार की सन्धियों के सर्वोत्तम उदाहरण सन् 1958 का सामुद्रिक विधि पर जिनेवा कन्वेंशन तथा सन 1969 का सन्धियों पर विधि का वियेना कन्वेंशन है।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि में विधि निर्माण करने वाली सन्धियों का वही स्थान है जो राष्ट्रीय विधि में विधायन (Legislation) का विधि का सृजन करने वाली सन्धियाँ वह साधन हैं जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विधि को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है तथा राष्ट्रों के मध्य नियम को पुष्ट किया जा सकता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ तभी सार्वभौमिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकती हैं जब आवश्यक राष्ट्रों या राज्यों का समर्थन सन्धियों को प्राप्त हो। आवश्यक राष्ट्रों से तात्पर्य उन राष्ट्रों से है जो वीटो का अधिकार रखते हैं जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन सन्धियों की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास का उपयोगी माध्यम है।
(2) संविदात्मक सन्धियाँ (Treaty Contracts) — विधि निर्मित करने वाली सन्धियाँ सार्वभौमिक तथा आवश्यक होती हैं जबकि संविदात्मक सन्धियाँ अर्थात् संविदा को जन्म देने वाली सन्धियाँ दो या अधिक राज्यों (राष्ट्रों) के मध्य होती हैं। इस प्रकार की सन्धियों के प्रावधान इस करार या संविदा के पक्षकारों पर बाध्य होते हैं। इस प्रकार की सन्धियाँ प्रधागत नियम के विकास से सम्बन्धित सिद्धान्तों को लागू करके अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में सहायता करती हैं। यह प्रथागत नियमों के अनुरूप किसी नियम को सन्धियों में सम्मिलित करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की सन्धि होने के पश्चात् कुछ और राष्ट्र (राज्य) इसी प्रकार की सन्धियाँ कर सकते हैं। उसमें यह कहा जा सकता है कि किसी नियम के अस्तित्व के साक्ष्यिक मूल्य के रूप में भी सन्धि का अपना महत्व है तथा यह बात विकास की स्वतन्त्र प्रक्रिया के द्वारा एक विधि के रूप में परिवर्तित हो चुकी है।
प्रश्न 5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध के बारे में विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। भारतीय न्यायालयों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की क्या स्थिति है?
Examine the different theories which explain the relationship between International Law and Municipal law. What is the position of International Law in Indian Courts?
उत्तर – अन्तर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों तथा उनके एक-दूसरे के मध्य व्यवहारों को नियन्त्रित करती है जबकि राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत उन नियमों को समाविष्ट किया गया है जिसके द्वारा उस विशिष्ट राष्ट्र के नागरिकों के आपसी व्यवहारों तथा सम्बन्धों को नियन्त्रित किया जाता है परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम किसी विशिष्ट राष्ट्र के नागरिकों को भी प्रभावित करते हैं। इस विषय में विचारणीय प्रश्न यह हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि (Municipal Law) के मध्य क्या सम्बन्ध है। इनके मध्य परस्पर विरोध होने पर क्या स्थिति होगी।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) तथा राष्ट्रीय विधि (Municipal Law). के मध्य सम्बन्धों (Relationship) को स्पष्ट करने हेतु कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।
ये कुछ सिद्धान्त निम्न हैं-
(1) अद्वैतात्मक सिद्धान्त (Monilism Theory)
(2) द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory)
(3) विशिष्ट ग्राह्यता का सिद्धान्त (Specific Adoption Theory)
(4) रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory)
(5) प्रत्यायोजन का सिद्धान्त (Delegation Theory) 1
(1) अद्वैतात्मक सिद्धान्त (Monilism Theory) – इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि संयुक्त विधि ज्ञान की दो शाखायें हैं जो समुदाय पर एक या दूसरे तरीके से लागू होती है। अद्वैतात्मक सिद्धान्त के लेखकों के अनुसार अन्तिम विश्लेषण में सभी विधियों के मूल में हम मनुष्य को ही पाते हैं तथा अन्तिम विश्लेषण में हम पाते हैं कि चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि हो या राष्ट्रीय विधि, विधियाँ मनुष्यों के लिए मनुष्यों द्वारा बनायी गयी हैं।
इस सिद्धान्त को मानने वाले सिविल विधि की अन्तिम संरचना के वैज्ञानिक विश्लेषण (Scientific analysis) पर बल देते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि एक ही कार्यप्रणाली (phenomenon) के रूप हैं। ये दोनों विधियाँ एक ही मौलिक नियम से ली गई हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में से केल्सन आदि ने कहा-एक नार यह स्वीकार कर लिया जाय कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक ऐसे नियमों की एक पद्धति है जिनका वास्तविक विधिक चरित्र है तब इस बात से इंकार करना असम्भव हो जायेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि उसी संयुक्त विधि विज्ञान का एक अंग भी है। राइट (Write), केल्सन तथा ड्यूगिट इस सिद्धान्त के मानने वाले विद्वान हैं।
अद्वैतात्मक सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य सभी विधियों के मूल में हैं, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता परन्तु यदि व्यवहार में देखा जाय तो स्वतन्त्र राष्ट्र इस सिद्धान्त का अनुपालन नहीं करते। स्वतन्त्र राष्ट्रों का यह तर्क होता है कि अन्र्तराष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि दोनों स्वतन्त्र विधि पद्धतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभु है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि से बाध्य नहीं है। राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने उस पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को तार्किक रूप से स्वीकार किया है।
(2) द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory) – इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में प्रमुख हैं ओपेनहाइम। ओपेनहाइम के अनुसार- राष्ट्रों की विधि (Municipal Law) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Intrnational Law) प्रधानतः एक-दूसरे से भिन्न तथा पृथक् हैं। ये विधियाँ पृथक् प्रथक् रूप से आपस में स्वयं पूर्ण हैं। इनमें एक-दूसरे के नियम एक दूसरी पद्धति में ग्रहण नहीं किये जाते हैं। अपने सिद्धान्त के समर्थन में इन विद्वानों का कहना है कि प्रथम तो इन विधियों के स्रोतों में ही अन्तर है तथा इसके अतिरिक्त हम पाते हैं कि राष्ट्रीय या नागरिक विधि राज्य के प्रभुत्व के अधीन व्यक्तियों के अथवा व्यक्तियों तथा राज्यों के सम्बन्धों को नियन्त्रित करती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों (राष्ट्रों) के या सदस्य राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध को नियन्त्रित करती है। इस सिद्धान्त को 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया गया है। इस शताब्दी में राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता तथा उनकी अपनी इच्छा या सहमति पर अधिक बल दिया गया। इस प्रकार द्वैतात्मक सिद्धान्त स्वतन्त्र राष्ट्रों के पूर्ण सम्प्रभुता पर आधारित है। इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादकों में ट्रीपेल तथा एंजीलाटी है। ट्रीपल का कहना है कि राष्ट्रीय विधि (Municipal Law) उस राष्ट्र के नागरिकों पर लागू होती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) स्वतन्त्र राष्ट्रों पर लागू होती है तथा राष्ट्रीय विधि का निर्माण उस राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सभी सदस्य राष्ट्रों की सामूहिक या सामान्य इच्छा होती है।
यह कहना सत्य नहीं है किं अन्तर्राष्ट्रीय विधि सिर्फ राष्ट्रों पर ही लागू होती है आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वतन्त्र राष्ट्रों, व्यक्तियों तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को भी प्रभावित करती है। वास्तव में राष्ट्रों की इच्छा अपने नागरिकों की इच्छा (Will) के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि को निर्मित करने वाले राष्ट्रों की इच्छा उनके नागरिकों की इच्छा को ही प्रतिलक्षित करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के मूल में नागरिकों की इच्छा ही होती है। एन्जीलोटी ने इसको दूसरे रूप में स्पष्ट करने की कोशिश की है।
ऐंजीलाटी का मत है कि राष्ट्रीय विधि में विधिक पवित्रता (Legal sanctity) है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अनुसरण इसलिए किया जाता है क्योंकि राज्य नैतिक रूप से उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य है।
(3) विशिष्ट ग्राह्यता का सिद्धान्त (Specific Adoption Theory)- सकारात्मक सिद्धान्त (positivist) के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रत्यक्ष रूप से (सीधे : Directly) राष्ट्रीय विधि के क्षेत्रों में लागू नहीं की जा सकती। इसे राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू करने से पूर्व राष्ट्रीय विधि के अनुरूप अपने आपको अपनाने योग्य (ग्राहा: adoptable) बनाना होगा। दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में तभी लागू की जा सकती है जब राष्ट्रीय विधि (Municipal Law) या तो उसे अपने अनुरूप ग्राह्य बना ले अथवा अपने क्षेत्र में लागू होने की विशिष्ट अनुमति दे। यह विचारधारा आमतौर पर स्वतन्त्र राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के सम्बन्ध में अनुसरित किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को विशिष्टतया अपनाया न जाय या उनमें कुछ परिवर्तन न किया जाय अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को ज्यों का त्यों राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का उल्लेख आवश्यक है जिन्हें भारतीय संसद ने अपनाया है। ये हैं-
(1) रंगभेद संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (Convention) अधिनियम, 1981,
(2) बलान्नयन विरोधी अधिनियम (Anti Hijacking Act), 1982
(3) नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध अवैध कार्य निरोधक अधिनियम, 1982 (Suppression of Unlawful Act Against Safety of Civil AviationAct, 1982)]
(4) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1882
यह विचारधारा इसलिए उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं को बिना विशिष्ट ग्राह्यता के राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू किया गया है।
(4) रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory)- इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में से स्टार्क एक थे। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों को राष्ट्रीय विधि (Municipal law) के क्षेत्र में लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बिना रूपान्तर या परिवर्तन के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को राष्ट्रीय विधि (Minicipal law) के क्षेत्र में लागू नहीं कराया जा सकता। इसके उदाहरण के रूप में हम ग्रेट ब्रिटेन द्वारा की गयी प्रत्यर्पण (Extradition) सन्धियों का उल्लेख कर सकते हैं।
परन्तु यह स्मरणीय है कि राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू होने के लिए सभी सन्धियों को रूपान्तरित होना आवश्यक नहीं है। कई विधि निर्माण करने वाली सन्धियों को बिना रूपान्तर के राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू किया गया है।
(5) प्रत्यायोजन का सिद्धान्त (Delegation Theory)- रूपान्तर सिद्धान्त के आलोचकों ने एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसे प्रत्यायोजन का सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संवैधानिक नियम प्रत्येक राष्ट्र (State) को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे यह निर्धारित करें कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में किस प्रकार तथा किस सीमा तक लागू होंगी। इस प्रकार प्रत्येक मामले में न तो ग्राह्यता, न तो रूपान्तर की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र के अपने संविधान में बतायी गई प्रक्रिया तथा विधि के अनुसार लागू की जाती है।
यह सिद्धान्त द्वैतवाद की प्रतिक्रिया के रूप में है। परन्तु यह सुनिश्चित नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की संवैधानिक विधि कहाँ है तथा इन तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संवैधानिक नियमों ने कब और किस प्रकार राष्ट्रीय संविधानों को शक्ति का प्रत्यायोजन कब और कैसे किया यह स्पष्ट नहीं है। यह सिद्धान्त इसलिए भी उपयुक्त नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु है तथा यह अपने ऊपर किसी शक्ति को मान्यता नहीं देता जो ऐसे राष्ट्रों की शक्ति का प्रत्यायोजन कर सके।
इस विषय में भारतीय न्यायालयों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थिति – अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य सम्बन्ध में भारतीय न्यायालयों की स्थिति को समझने के लिए हमें संविधान लागू होने के पूर्व तथा संविधान लागू होने के बाद की स्थिति का अध्ययन करना होगा। संविधान लागू होने से पूर्व भारतीय न्यायालय ब्रिटिश प्रचलन से बाध्य थे। ब्रिटिश प्रचलन के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत नियम तथा सन्धियों द्वारा प्रतिपादित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि में भिन्नता की जाती है।
संविधान अपनाने के पश्चात् इस विषय में सभी कुछ संविधान के प्रावधानों पर निर्भर है। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य निम्नलिखित को नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार पूरा करने का प्रयत्न करेगा-
(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना;
(2) राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्माननीय सम्बन्धों को बनाये रखना;
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि के आभारों (obligations) के प्रति संगठित लोक के पारस्परिक व्यवहारों के प्रसंग में सम्मान की भावना उत्पन्न करना;
(4) मध्यस्थ निर्णयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने को प्रोत्साहन देना।
स्टेट ऑफ मद्रास बनाम जी० जी० मेनन (1954) सु० को० 517 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1903 को भारतीय संसद ने अपना लिया (adopt) है। इस प्रकार इस अधिनियम के प्रावधानों को भारत में इस अधिनियम के प्रावधानों में उचित परिवर्तन कर भारत में लागू होने योग्य बनाया जाना चाहिए। 1903 के प्रत्यर्पण अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने परिवर्तन के साथ अपना लिया है परन्तु Fugitive Offenders Act भारतीय संसद ने अधिनियम पारित कर अपनाया नहीं है। अतः यह अधिनियम भारत में लागू नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस वाद में ग्राह्यता के सिद्धान्त (adoptive theory) को मान्यता दी गयी है।
ग्रामोफोन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० बनाम विरेन्द्र बहादुर पाण्डेय, ए० आई० आर० 1984 सु० को० 66 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति चिनप्पारेड्डी ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के बारे में संसद ने ग्राह्यता से इन्कार कर दिया है तो राष्ट्रीय न्यायालय (National Court) इसे लागू नहीं कर सकते। राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को तभी लागू कर सकते हैं यदि वे राष्ट्रीय विधि के नियमों के प्रतिकूल या प्रतिरोध में नहीं हैं। यदि किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि में विरोध या प्रतिकूलता है तो राष्ट्रीय विधि मान्य होगी।
विशाका बनाम राजस्थान राज्य, ए० आई० आर० 1997 सु० को 3011 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नौकरी करने वाली महिलाओं के उनके कार्यस्थल में उनके विरुद्ध सम्भोग संताप को रोकने के प्रभावशाली उपाय के सम्बन्ध में घरेलू विधि की अनुपस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 तथा 21 में उल्लिखित मानव गरिमा के साथ लैंगिक समानता के अधिकार की गारण्टी का निर्धचन करने की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय ने ऐपेरेल एक्सपोर्ट कारपोरेशन प्रोमोशन काउन्सिल बनाम ए० के० चोपड़ा, ए० आई० आर० 1997 सु० को० के वाद में कर दिया गया।
इस प्रकार भारतीय न्यायालयों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है-
(1) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत नियम को अधिसंख्य राज्यों ने देशी विधि का अंग माना है तथा यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं हैं तो ग्राहाता (adoption) की आवश्यकता नहीं है।
(2) कुछ राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत नियम को राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा. विशिष्ट ग्राह्यता (specific adoption) के अभाव में भी लागू किया जाता है।
(3) जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू करने का प्रश्न है, सभी राष्ट्रों द्वारा एकरूपता नहीं अपनायी जाती।
(4) अधिसंख्य राष्ट्रों में यद्यपि न्यायालय राष्ट्रीय विधि को ही प्रमुखता देते हैं तथा यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन हुआ है तो यह मामला राजनयिक स्तर (Diplomatic level) पर निपटाया जाना चाहिए।
प्रश्न 6. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध के विषय में राज्यों के अभ्यास के बारे में संक्षेप में बताइये।
Explain in brief the practice of states regarding relationship between International Law and National Law.
उत्तर – अन्तर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के विषय में राज्यों के अभ्यास (Practice of State Regarding Relationship) – राज्यों के अभ्यास से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उस सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं, जिसे वे स्वयं अपनी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली के अनुसार अधिक समुचित समझते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि रूढ़िगत तथा सन्धिजात को राज्यों द्वारा किस सीमा तक लागू किया जाता है, इस सम्बन्ध में राज्य अभ्यास भिन्न-भिन्न हैं। कुछ राज्यों के अभ्यास निम्न प्रकार हैं-
(1) ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) – ग्रेट ब्रिटेन में, रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा सन्धियों को भिन्न-भिन्न रूप से लागू किया जाता है। अतः उनकी विवेचना पृथक् रूप से की गयी है-
(क) रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Customary Intarnational Law)- इस सिद्धान्त को कई मामलों में लागू किया गया है। लेकिन आर० बनाम केन (R. v. Keyn) के मामले में न्यायमूर्ति काकबर्न (Justice Cockburn) ने इस सिद्धान्त से भिन्न मत व्यक्त किया। इस मामले में निर्णय दिया गया कि रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि देश की विधि का भाग तभी बनेगी, जब उसे स्पष्ट रूप से विधायन, न्यायिक विनिश्चय (Judicial Decisions) या स्थापित प्रथा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया हो। इस मामले में जो सिद्धान्त बनाया गया है, उसे स्थानान्तरण के सिद्धान्त (Doctrine of Transformation) के नाम से जाना जाता है, अर्थात् न्यायालयों द्वारा रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के पूर्व उसे इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय विधि में रूपान्तरित होना आवश्यक है। बाद में 1905 में लार्ड अल्बरस्टोन (Lord Alverstone) ने वेस्ट रैण्ड सेन्ट्रल गोल्ड माइनिंग कम्पनी बनाम आर० में समावेश (Incorporation) के सिद्धान्त की फिर से पुष्टि की।
(ख) सन्धियाँ (Treaties) सन्धियों को लागू करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश अभ्यास प्रमुख रूप से संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। कुछ सन्धियाँ न्यायालयों पर केवल उस समय बाध्यकारी होती हैं, जब संसद द्वारा उस सन्धि से सम्बन्धित अधिनियम पारित कर दिये जाते हैं। यह नियम उन सन्धियों पर लागू होता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित करती हैं, या जो आर्थिक बाध्यताओं को आरोपित करती हैं, या जो न्यायालयों में उनके प्रवर्तन के लिए कॉमन विधि (Common Law) या स्टैट्यूट्स के संशोधन की अपेक्षा करती हैं।
(2) संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) अमेरिका में भी रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा सन्धियों को भिन्न-भिन्न रूप से लागू किया जाता है-
(क) रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Customary International Law)- जहाँ तक रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध है, अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा स्थिति अधिक स्पष्ट है। जिस रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सार्वभौमिक रूप से मान्यता मिल गयी है और जिसे संयुक्त राज्य की सम्मति प्राप्त हो गयी है, वह अमेरिकी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है तथा उनके द्वारा लागू की जाती है।
मैक्लीओड बनाम यूनाइटेड स्टेट्स (Macleod v. United States) में न्यायालयों ने कहा था कि स्टैट्यूट्स का अर्थान्वयन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों की सीमाओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, जिसका अनुपालन राष्ट्रों की शान्ति तथा मैत्री के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन यदि कोई कानून अस्तित्व में है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम से विरोध है, तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम पर स्टैट्यूट्स अभिभावी होगा।
(ख) सन्धियाँ (Treaties)- जहाँ तक सन्धियों का सम्बन्ध है, अमेरिकी अभ्यास ब्रिटिश अभ्यास से भिन्न हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 का खण्ड 2 प्रावधान करता है कि ” सभी सन्धियाँ जो संयुक्त राज्य के प्राधिकार के अधीन की जायेंगी, देश की सर्वोच्च विधि होंगी।” (All Treaties made, or which shall be made under the authority of the United States shall be the Supreme law of the Land) ।
(3) सोवियत अभ्यास (Soviet Practice) – सोवियत रूस में राष्ट्रीय विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को एक-दूसरे के अधीनस्थ नहीं बल्कि दो पृथक् विधिक प्रणाली माना जाता था। सोवियत संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार, अन्य राज्यों के साथ सोवियत रूस का सम्बन्ध निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित था-
प्रभुत्वसम्पन्नता समता, बल की धमकी या प्रयोग का पारस्परिक परित्याग, सीमाओं का उल्लंघन न किया जाना, राज्यों की राज्य क्षेत्रीय अखण्डता, विवादों का शान्तिपूर्ण निपटारा, आन्तरिक मामलों में मध्यक्षेप न किया जाना, मानव अधिकारों तथा मूल स्वतन्त्रताओं के लिए सम्मान, लोगों के समान अधिकार तथा अपनी नियति को स्वयं निश्चित करने के उनके अधिकार, राज्यों के मध्य सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतः मान्य सिद्धान्तों तथा नियमों से उत्पन्न बाध्यताओं को सद्भावपूर्वक पूरा करना।
(4) यूरोपीय राज्यों में अभ्यास (Practice in European States)- यूरोपीय राज्यों में से अधिकतम राज्य ग्रेट ब्रिटेने की तरह रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समावेशन या अंगीकरण (Incorporation or Adoption) के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं। अधिकतम राज्यों ने अपने संविधान में समुचित प्रावधानों को समाविष्ट किया है। जहाँ तक सन्धियों का सम्बन्ध है, कई देश इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं कि संविधान के अनुसार की गयी सन्धियाँ समावेशन के किसी विनिर्दिष्ट कार्य (Specific Act) के बिना न्यायालयों पर आबद्ध होती हैं।
(5) लैटिन अमेरिकी राज्यों में अभ्यास (Practice in Latin American States)- लैटिन अमेरिकी राज्यों ने सभी राज्यों से अपने संविधानों तथा अन्य राष्ट्रीय विधियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आवश्यक सिद्धान्तों का समावेशन के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
(6) भारतीय अभ्यास (Indian Practice)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन विश्व के प्रति भारत की सामान्य बाध्यता के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, राज्य यह प्रयास करेगा कि (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की वृद्धि हो; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बने रहें; (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बाध्यताओं को राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार में आदर मिले; और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन मिले। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है जो राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को प्रतिपादित करता है।
अनुच्छेद 51 में ‘अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ तथा सन्धि बाध्यताओं शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि शब्द “अन्तर्राष्ट्रीय विधि” रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को निर्दिष्ट करता है। इसका यह तात्पर्य हो सकता है कि अनुच्छेद 51 रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा संधिबद्ध विधि को एक समान मानता है फिर भी रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लागू होने की विवेचना पृथक् रूप से की जा रही है-
(क) रूढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Customary Intarnational Law)- भारतीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रूढिगत नियमों को लागू करेंगे, यदि उन पर राष्ट्रीय विधि के स्पष्ट नियम अभिभावी नहीं होते हैं। श्री कृष्ण शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए० आई० आर० 1954 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय न्यायालय आन्तरिक विधि (राष्ट्रीय विधि) के उन नियमों को लागू करेंगे जो (क) भारतीय संविधान, (ख) भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित परिनियम और (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित परिनियमों में सम्मिलित हैं।
ग्रोमोफोन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० बनाम बीरेन्द्र बहादुर पाण्डेय, में उच्चतम न्यायालय का अवलोकन (Observance) अन्तर्राष्ट्रीय विधि क्रे रूढ़िगत नियमों के बाध्यकारी बल (Binding Force) से सम्बन्धित था।
(ख) सन्धियाँ (Treaties)- भारत में सन्धियों के सम्बन्ध में यह मत है कि सन्धियाँ उस समय बाध्यकारी होंगी जब विधान द्वारा उससे सम्बन्धित नियम पारित हो जाये। यह मत संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है जो प्रावधान करता है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गयी किसी सन्धि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किये गये विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।
सिविल राइट्स विजिलेन्स कमेटी, बंगलौर बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1983 के बाद में यह प्रश्न था कि बायकाट तथा कुक (Boycott and Cook) दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत में आने की तथा दक्षिण अफ्रिका जो रंग भेद (Apartheid) की नीति को मान्यता देती थी, के साथ उनके सम्बन्धों के कारण भारत के विरुद्ध इंग्लिश क्रिकेट को दल के सदस्य के रूप में मैच खेलने की अनुमति दी जायेगी। याची ने तर्क दिया कि इन दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को भारत में प्रवेश देने तथा भारत में क्रिकेट खेलने की अनुमति देने की भारत सरकार की कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी सदस्यता से सम्बन्धित ग्लेनोगिल्स (Gleneagles) समझौता इसकी बाध्यताओं का उल्लंघन है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संयुक्त राष्ट्र की इसकी सदस्यता से सम्बन्धित ग्लेनीगिल्स समझौता (Gleneagles Accord) तथा बाध्यताओं के अधीन भारत सरकार की वाध्यता को इस देश के नागरिकों या ऐसे नागरिकों के संगठनों के निर्देश पर, भारत में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यदि ऐसी बाध्यताओं को समुचित विधायन के माध्यम से इस देश की विधि का भाग नहीं बना दिया जाता।
विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए० आई० आर० (1999) सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि किसी भी कार्य स्थानों में काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय विधि नहीं है अतः अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानकों पर ध्यान देना चाहिए जब उनके मध्य में कोई असंगतता न हो और राज्य विधि में शून्यता हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न की प्रत्येक घटना से लैंगिक समानता के मूल अधिकार तथा प्राण व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। चूंकि भारत में न तो सिविल और न ही दाण्डिक विधि में कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न के लिए कोई प्रावधान है अतः अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानक को ध्यान में रखकर यह कहा गया है कि लैंगिक समानता तथा मानव गरिमा के साथ काम करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 (1) और 21 में विवक्षित है।
प्रश्न 7. मान्यता की परिभाषा दीजिए। मान्यता के निर्माणात्मक तथा घोषणात्मक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
अथवा
“कोई राज्य केवल एवं अनन्य रूप से मान्यता से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है एवं होता है।” इस कथन की समीक्षा करते हुए मान्यता के सिद्धान्तों का वर्णन करें।
Define recognition. Describe the constitutional and declaratory theory of recognition.
Or
“Only and exclusively by recognition any state is a International person and become.” Elucidate this with theories of recognition?
उत्तर- मान्यता का अर्थ- विश्व विभिन्न राष्ट्रों का एक समुदाय है जिसमें विभिन्न सम्प्रभु राष्ट्र एक-दूसरे की सम्प्रभुता को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रों की सम्प्रभुता को स्वीकार करना परस्पर सहअस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रो० एल० ओपेनहाइम के अनुसार अन्तराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में एक राष्ट्र को मान्यता देकर, एक अस्तित्वाधीन राष्ट्र यह घोषणा करता है कि उनके विचार में एक राष्ट्र (जिसे मान्यता दी जा रही है) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वांछित राष्ट्रीयता (राष्ट्र होने) की शर्तें पूरी करता है। फेन्विक ने भी उपरोक्त विचार की पुष्टि की है। फेन्विक के अनुसार मान्यता के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य औपचारिक रूप से अभिस्वीकृति करता है कि नये राष्ट्र या राज्य ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी है।
प्रो० केल्सन के अनुसार किसी समुदाय को मान्यता प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन निम्न शर्तों को पूरा करना होगा-
(1) उस समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए।
(2) उसे निश्चित सीमा क्षेत्र पर नियन्त्रण प्राप्त होना चाहिए।
(3) यह नियन्त्रण स्थायित्व की ओर होना चाहिए।
(4) इस प्रकार संगठित समुदाय स्वतन्त्र होना चाहिए।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि यह नहीं बताती कि यह कैसे पता लगाया जाय कि कोई राज्य या राजनीतिक संगठन मान्यता की उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विवेक पर यह निर्धारित करने का दायित्व छोड़ती है कि क्या किसी मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य मान्यता की या राष्ट्र होने की आवश्यक शतों को पूरा करता है अथवा नहीं। इसी कारण से मान्यता एक राजनीतिक कार्य है।
राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देने के विषय में दो सिद्धान्त प्रचलित है।
(1) संगठनात्मक (Constitutive) सिद्धान्त; तथा
(2) घोषणात्मक (Declarative) सिद्धान्त या साक्ष्यात्मक (Evidentiary) सिद्धान्त।
(1) संगठनात्मक सिद्धान्त (Constitutive Theory) – इस सिद्धान्त के अनुसार मान्यता के कार्य से मान्यता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत कर्त्तव्य तथा अधिकार प्रदान किये जाते हैं। मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय राष्ट्रों के परिवार का एक सदस्य बनकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। संगठनात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं- हिगेल, एन्जीलोटी तथा ओपेनहाइम। प्रो० ओपेनहाइम के अनुसार- “मान्यता से ही तथा सिर्फ मान्यता के कारण ही एक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनता है तथा मान्यता से ही एक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है।” हालैण्ड ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। हालैण्ड के अनुसार मान्यता एक राष्ट्र या राज्य को परिपक्वता (Maturity) प्रदान करता है तथा जब तक एक राष्ट्र या राज्य मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत उसे अधिकार प्राप्त नहीं होता।
राष्ट्रों (राज्यों) के व्यवहार इसके प्रतिकूल हैं। इस सिद्धान्त की आलोचना यह कहकर भी की गई है कि यदि किसी राज्य ने राष्ट्र होने के सभी गुण प्राप्त कर लिये हैं तो वर्तमान राज्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसे मान्यता प्रदान करें। यह विचार सही नहीं है क्योंकि व्यवहारतः राज्य इस प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करते। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी राष्ट्र को मान्यता नहीं मिलती तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत न तो अधिकार प्राप्त होते हैं न कर्तव्य, यह विचार भी सही नहीं है। यह उस परिस्थिति में अर्थहीन हो जाता है जहाँ एक राष्ट्र को कुछ अस्तित्वाधीन राष्ट्र मान्यता देते हैं परन्तु कुछ राष्ट्र मान्यता नहीं देते। यदि उपरोक्त विचार मान लिया जाय तो कठिनाई उत्पन्न होगी। उदाहरण के रूप में बंगलादेश को कुछ वर्षों तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी थी या चीन को काफी वर्षों तक अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि बंगलादेश या चीन इन वर्षों के दौरान अधिकार या कर्तव्य नहीं रखते थे।
(2) घोषणात्मक सिद्धान्त (Declaratory Theory)- इस सिद्धान्त के अनुसार नवीन सरकार को अधिकारिता तथा राष्ट्रीयता (Statehood) मान्यता से पृथक् तथा मान्यतापूर्ण अस्तित्व में होती है। मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा पूर्व विद्यमान तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार मान्यता का कार्य इस वर्तमान या विद्यमान तथ्य की घोषणा मात्र है कि एक विशिष्ट राष्ट्र या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वांछित आवश्यक गुणों से युक्त है या एक राष्ट्र या सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वांछित गुण हैं। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में हाल, वेगनर, ब्रायरली पिट कोबेट तथा फिशर हैं। ब्रायरली के अनुसार, “एक नवीन राष्ट्र को मान्यता प्रदान करना एक संगठनात्मक (Constitutive) कार्य न होकर घोषणात्मक (Declaratory) कार्य है।” एक राष्ट्र या राज्य मान्यता के अभाव में भी अस्तित्व में रहता है तथा यदि वास्तव में राज्य का अस्तित्व है तो उसे राष्ट्र के रूप में व्यवहार किये जाने को अधिकार है चाहे उसे अन्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता दी जाय या न दी जाय। सोवियत व्यवहार तथा नियम भी घोषणात्मक सिद्धान्त के अनुरूप हैं जिनके अनुसार राज्य का जन्म एक आन्तरिक विधि का कार्य है न कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का। आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता का मोहताज नहीं है।
इस सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर की गई है कि भले ही एक राष्ट्र का अस्तित्व मान्यता के पूर्व होता है परन्तु मान्यता एक ऐसा कार्य है जिसका अपना विधिक प्रभाव होता है तथा वह विधिक प्रभाव संगठनात्मक प्रकृति का ही होता है।
सारांश- अब यह देखना है कि मान्यता घोषणात्मक कार्य है या संगठनात्मक। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मान्यता का कार्य घोषणात्मक तथा संगठनात्मक दोनों है। यह दोनों सिद्धान्त अपने आप में सत्य हैं। इस प्रकार हम न्यायमूर्ति लाटरपैट के शब्दों में कह सकते हैं कि पहले संगठनात्मक सिद्धान्त के अनुसार यह देखना होगा कि जिस राष्ट्र को मान्यता प्रदान की जा रही है वह राष्ट्र एक प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र के आवश्यक गुण से युक्त है अथवा नहीं। यह सुनिश्चित हो जाय कि एक राष्ट्र के पास राष्ट्र या स्वतन्त्र सरकार के सभी गुण विद्यमान हैं तो उसे घोषणात्मक कार्य द्वारा मान्यता देनी चाहिए तथा इस घोषणा के द्वारा ही वह राज्य मान्यता प्रदान करने वाले देश की दृष्टि में एक सम्प्रभु राष्ट्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। इस प्रकार इसी घोषणात्मक कार्य द्वारा कुछ विधिक परिणामों को संगठित या निर्मित (constitute) किया जाता है। ओपेनहाइम, जो संगठनात्मक सिद्धान्त के समर्थकों में से हैं, ने भी स्वीकार किया है कि मान्यता एक अस्तित्वाधीन या विद्यमान तथ्य की घोषणा है परन्तु यह संगठनात्मक (constitutive) प्रकृति का है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मान्यता का कार्य एक संगठनात्मक कार्य है जिसकी घोषणा कर मान्यता प्रदान करने वाला देश उसे विधिक प्रभाव देता है। एक बार ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर से यह पूछा गया कि वे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता क्यों नहीं दे रही हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम देश (राष्ट्र) को मान्यता देते हैं न कि किसी संगठन को (We recognise nation not organisation) l
इस प्रकार आमतौर पर कोई राष्ट्र किसी को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक उसके विचार में उस राष्ट्र के पास वे सभी गुण नहीं हैं जो एक राष्ट्र होने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार संगठनात्मक सिद्धान्त के अनुसार मान्यता तभी दी जा सकती है जब मान्यता देने वाला राष्ट्र यह सुनिश्चित कर ले कि जिस राष्ट्र को मान्यता तभी दी जा सकती है उसके पास एक सम्प्रभु राष्ट्र के सभी गुण विद्यमान हों तथा यदि यह सुनिश्चित हो जाय तो उसकी घोषणा करके उसे विधिक प्रभाव दिया जाता है। अतः मान्यता का कार्य संगठनात्मक भी है तथा घोषणात्मक भी। परन्तु कभी-कभी एक राष्ट्र के पास राष्ट्र होने के गुण विद्यमान होने के बाद भी उसे मान्यता नहीं दी जाती अतः यह कहा जा सकता है कि मान्यता का कार्य राजनीतिक भी है।
प्रश्न 8. तथ्येन मान्यता तथा विधितः मान्यता को समझाते हुए इनमें अन्तर स्पष्ट करें। Describe the de facto and de jure recognition. Differentiate between the two?
उत्तर- मान्यता के दो प्रकार होते हैं-
(1) वस्तुतः मान्यता (de facto), तथा
(2) विधितः मान्यता (de jure) ।
(1) वस्तुतः मान्यता (de facto recognition) – जब विद्यमान राज्य यह समझते हैं कि नये राज्य ने पर्याप्त स्थायित्व ग्रहण नहीं किया है, तब वे उसे औपबन्धिक रूप से
(Provisionally) मान्यता प्रदान कर सकता है। इस मान्यता को वस्तुतः मान्यता कहा जाता है।
ओपेनहाइम के शब्दों में “वस्तुतः मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के विचार में, यद्यपि नया राज्य वास्तव में स्वतन्त्र है तथा उसके अधीन राज्य क्षेत्र में शासन करने की उसकी प्रभावी शक्ति है, फिर भी उसने पर्याप्त स्थायित्व अर्जित नहीं किया है या मान्यता की अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन करने की सम्भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया है।”
“De-facto recognition takes place when, in the view of recognizing State, the new authority, although actually independent and wielding effective power in the territory under its control, has not acquired sufficient stability or does not as yet offer prospects of complying with other requirements of recognition.” op. cit. p. 155.
सामान्य रूप से वस्तुतः मान्यता तब प्रदान की जाती है जब मान्यता देने वाला राज्य यह समझता है कि यद्यपि नये राज्य के पास सम्मत सरकार है, फिर भी राज्य क्षेत्र को शासित करने की उसकी क्षमता या निरन्तरता संदेहास्पद है। वस्तुतः मान्यता देने वाले राज्य की ओर से नये राज्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा दर्शाता है, किन्तु इच्छा औपबन्धिक रूप से राजत्व के सभी तत्वों की पूर्ति के अध्यधीन दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः मान्यता का सही उद्देश्य यह घेषणा करना है कि नये राज्य की सरकार होने का दावा करने वाला निकाय वास्तव में पूर्णतः विधितः मान्यता की ओर प्राथमिक कदम के रूप में अन्य शर्तों की पुष्टि किये बिना प्रभावी प्राधिकार धारण करता है। यदि ये शर्तें बाद में पूरी हो जाती हैं, तो पूर्ण विधितः मान्यता दे दी जायेगी किन्तु, यदि स्थायी रूप से उनका अभाव बना रहता है, तो मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी या वापस ले ली जायेगी। अतः वस्तुतः मान्यता विधितः मान्यता के रूप में पहला कदम माना जा सकता है। ब्रिटेन द्वारा सोवियत संघ को 16 मार्च, 1921 को वस्तुतः तथा बाद में 1 फरवरी, 1924 को विधितः मान्यता प्रदान की गयी थी। चीन को भी बहुत से देशों ने काफी वर्षों तक केवल तथ्येन-मान्यता प्रदान की थी।
यदि विद्यमान राज्य वस्तुतः मान्यता प्रदान करने के बाद, बाद में विधितः मान्यता प्रदान करता है, तो विधि की मान्यता का प्रभाव भूतलक्षी तिथि, अर्थात, उस तिथि से होगा, जब वस्तुतः मान्यता प्रदान की गयी थी। लेकिन वस्तुतः मान्यता का प्रभाव वैसा नहीं है, जैसा कि विधितः मान्यता का है। सामान्यतया, तथ्य रूप से मान्यता प्राप्त राज्य से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये जाते हैं। पुनः, वस्तुतः मान्यता प्राप्त राज्यों के प्रतिनिधि को मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजनयिक उन्मुक्तियाँ नहीं प्राप्त होतीं। लेकिन इस सम्बन्ध में ‘राज्यों के अभ्यास एक समान नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभ्यास के अनुसार, वस्तुतः मान्यता प्राप्त सरकार के प्रतिनिधि राजनयिक उन्मुक्तियों का उपयोग करते हैं।
(2) विधितः मान्यता (De-Jure Recognition)- जब वर्तमान राज्य यह समझते हैं कि नया राज्य स्थायित्व तथा स्थिरता सहित राज्यत्व के सारे आवश्यक गुणों को धारण करने में सक्षम है तथा इसको जनसंख्या का समर्थन प्राप्त है, तब दी गयी मान्यता को विधितः मान्यता के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, विधितः मान्यता अन्तिम होती है। उदाहरण के लिए जब इसराइल राज्य बना तब अमेरिका तथा अन्य कई राज्यों ने उसको पूर्ण (full) मान्यता दी जिसको विधितः मान्यता कहा गया। विधितः मान्यता वस्तुतः मान्यता को दिये बिना भी दी जा सकती है। जब नया राज्य शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीके से अस्तित्व में आता है तब विधितः मान्यता दी जा सकती है। लेकिन जब राज्य क्रान्ति के माध्यम से गठित होता है तब कभी-कभी विधितः मान्यता वस्तुतः मान्यता के बाद दी जाती है।
तथ्यतः मान्यता एवं विधितः मान्यता (De jure and De facto Recognition) में अन्तर –
तथ्यतः मान्यता
(1) तथ्यतः मान्यता अन्तरिम प्रकृति की होती है।
(2) तथ्यतः मान्यता ऐसी शर्तों के अधीन दी जाती है जिसे मान्यता प्राप्त करने वाले राष्ट्र को पूरा करना होता है।
(3) तथ्यतः मान्यता के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि एक राष्ट्र, जिसे मान्यता दी जानी है, का अस्तित्व है तथा उसमें राष्ट्र होने के गुण विद्यमान हैं।
(4) तथ्यतः मान्यता, मान्यता की दिशा में प्रथम कदम है।
(5) जिस राष्ट्र ने सिर्फ तथ्यतः मान्यता प्राप्त की है उसके द्वारा स्थापित कम्पनी या उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार कम से कम उस देश से नहीं कर सकते जिसने सिर्फ तथ्यतः मान्यता प्रदान की है।
(6) जिस राष्ट्र को सिर्फ तथ्यतः मान्यता मिली है उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित उस राष्ट्र की सम्पत्ति से उस राष्ट्र को वंचित किया जा सकता है।
विधितः मान्यता
(1) विधिक मान्यता स्थायी प्रकृति की होती है।
(2) विधितः मान्यता राष्ट्र होने की आवश्यक शर्तों की पूर्ति की संतुष्टि के पश्चात् प्रदान की जाती है।
(3) विधितः मान्यता के द्वारा इस तथ्य को मान्यता दी जाती है कि जिस राष्ट्र को विधितः मान्यता दी जानी है उसमें अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को वहन करने की क्षमता है।
(4) विधितः मान्यता, मान्यता की कार्यवाही को पूर्ण करता है उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है।
(5) विधितः मान्यता प्राप्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित कम्पनियाँ तथा निगम अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार कर सकती हैं।
(6) विधितः मान्यता प्राप्त राष्ट्र को ऐसी सम्पत्ति, जो उसके सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित है, से वंचित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 9. “मान्यता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। क्या मान्यता एक राजनीतिक कार्य है या राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करती है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।
Describe the various forms of Recognition. Is recognition a political act or depends on the discretion of the state. Discuss this statement.
उत्तर- मान्यता के रूप (Forms of Recognition)- किसी राज्य को दो प्रकार से मान्यता दी जा सकती है-
(1) अभिव्यक्त मान्यता; तथा
(2) विवक्षित मान्यता।
(1) अभिव्यक्त मान्यता (Express Recognition) – जब विद्यमान राज्य कुछ औपचारिक घोषणा करके नये राज्य को मान्यता देते हैं, तब ऐसी घोषित मान्यता को अभिव्यक्त मान्यता कहा जाता है। जैसे- भारत द्वारा 6 दिसम्बर, 1971 को बंगला देश की मान्यता अभिव्यक्त मान्यता का उदाहरण है।
(2) विवक्षित मान्यता (Implied Recognition)- जब विद्यमान राज्य नये राज्य के मान्यता के सम्बन्ध में कोई औपचारिक घोषणा न कर कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे नये राज्य को मान्यता देने का आशय निर्दिष्ट होता है, तो इसे विवक्षित मान्यता कहते हैं। मान्टेवीडियो अभिसमय, 1933 के अनुच्छेद 7 के अधीन कहा गया है कि विवक्षित मान्यता उस कार्य का परिणाम है, “जो नये राज्य के मान्यता के आशय में निहित है।” इस प्रकार की मान्यता को विवक्षित मान्यता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। मान्यता का आशय राज्यों द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है।
(क) एकपक्षीय कार्य (Unilateral Acts) – जब कोई राज्य बिना मान्यता प्राप्त राज्य से द्विपक्षीय सन्धि करता है या राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करता है, तब यह आशय निकाला जा सकता है कि उसने नये राज्य को मान्यता प्रदान कर दी है।
(ख) सामूहिक कार्य (Collective Act) – ऐसा कहा जाता है कि नये राज्य को विद्यमान राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से मान्यता दी जा सकती है। यह तब होता है जब बिना मान्यता प्राप्त राज्य बहुपक्षीय सम्मेलन में या बहुपक्षीय सन्धि में भाग लेता है, तब यह माना जाता है कि सम्मेलन या सन्धि के अन्य पक्षकारों ने नये राज्य को मान्यता दे दी है। इसी प्रकार, जब नया राज्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनता है, तब यह माना जाता है कि संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा मान्यता प्रदान करने का संकेत दे दिया गया है। इस प्रकार की मान्यता को सामूहिक मान्यता कहा जाता है, क्योंकि राज्य को संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।
“क्या मान्यता एक राजनीतिक कार्य है या राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करती है”- मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नये राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जेसप के अनुसार “मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा वह यह स्वीकार करता है कि किसी राजनैतिक इकाई में राष्ट्रतत्व के आवश्यक गुण विद्यमान हैं, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मान्यता द्वारा उसे प्रदान करने वाले राज्य द्वारा मान्यता दिये जाने वाले राज्य के राष्ट्रत्व के तत्वों को स्वीकार किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि यह नहीं स्पष्ट करती है कि इन आवश्यक तत्वों का क्या मापदण्ड होगा अर्थात् कैसे यह पता चलेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रत्व के सभी तत्व उपस्थित हैं। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राज्यों को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वह स्वयं निश्चय करें कि जिस राज्य को वे मान्यता प्रदान कर रहे हैं उसमें राज्य के आवश्यक तत्व हैं अथवा नहीं। किसी नये राज्य या सरकार, से राजनीतिक या अन्य सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। यह प्रश्न कि क्या मान्यता एक राजनीतिक कार्य है या राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करती है तो सकारात्मक उत्तर यही होगा कि यह राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि यह स्पष्ट नहीं करती है कि यह कैसे निश्चित किया जायेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रत्व के गुण मौजूद हैं वास्तव में यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के स्वविवेक पर ही आधारित होता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्य स्तर पर ही आधारित है कि राज्य यह निश्चय करें कि किसी राज्य में राष्ट्रत्व के गुण विद्यमान हैं, या नहीं। प्रो० स्वार्जनबर्जर के अनुसार, “स्थापित नियमों तथा सन्धि-उत्तरदायित्वों की अनुपस्थिति में मान्यता एक स्वविवेक का प्रश्न है।”
लाटर पैट का कहना है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रत्व के गुण मौजूद हों तो दूसरे राष्ट्रों का यह कर्त्तव्यं हो जाता है कि वे उसे मान्यता प्रदान करें, यह राज्य के अभ्यास पर आधारित नहीं है। लाटर पैट का यह मत उचित प्रतीत होता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस प्रकार का कोई कार्य या उत्तरदायित्व राज्यों पर नहीं लादती है। राज्य मान्यता के विषय में कोई कर्त्तव्य नहीं मानते। अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी इस विषय में राज्य को बाध्य नहीं करती। मान्यता प्रदान करने के कार्य को बहुधा राजनीतिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है।
एडवर्ड कालिन्स के अनुसार- राज्यों तथा इनकी सरकार को मान्यता प्रदान किये जाने के विषय में राज्यों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक कार्य है। प्रो० लवान्टीन का कहना है कि मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे कमजोर कड़ी है क्योंकि इससे मान्यता प्रदान किये जाने वाले की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और उसके भौतिक स्रोतों में वृद्धि होती है। प्रायः सहानुभूति रखने वाले राज्यों द्वारा मान्यता या तो परिपक्वता आने के पूर्व दी जाती है या सहानुभूति रखने वाले राज्यों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। न दिये जाने का कार्य मान्यता प्रदान करने
अतः किसी राज्य को मान्यता दिये जाने या न दिये जाने का कार्य मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करता है। राज्य हमेशा अपने हितों के अनुसार ही कार्य करता है।
समय पूर्व या अपरिपक्व मान्यता प्रदान करना आमतौर से अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन नहीं है क्योंकि मान्यता प्रदान करने या न करने के सम्बन्ध में राज्यों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है यह राज्यों की स्वेच्छा तथा विवेक पर निर्भर करता है परन्तु यदि सुरक्षा परिषद् या महासभा यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके किसी राज्य को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में मना करती है तो राज्य को ऐसी मान्यता अनुज्ञेय होगी।
इस प्रकार फिलिप मार्शल ब्राउन ने मत प्रकट किया कि किसी नये राज्य की सरकार को मान्यता दिया जाना एक राजनयिक कार्य है न कि विधि सम्बन्धी।
सुझाव – इस सन्दर्भ में फिलिप सी० जोसेफ एक सुझाव यह देते हैं कि किसी नये राज्य में राष्ट्रत्व के गुण विद्यमान होने का मामला सामूहिक निर्णय के अधीन होना चाहिए। उनके अनुसार, सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर महासभा को घोषणा करनी चाहिए कि किसी राजनीतिक समुदाय में राष्ट्र के गुण मौजूद हैं या नहीं। जब तक इसकी घोषणा न हो जाय। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का निषेध होना चाहिए कि वे राजनीतिक समुदाय को मान्यता न दें। इस प्रकार नये राज्यों की मान्यता के विषय में संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार स्थापित राज्यों को चलना होगा।
यहाँ यदि इन सुझावों को माना जाय तो मान्यता में राज्यों की स्वेच्छा समाप्त होकर यह अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक नियन्त्रण के अधीन हो जायेगा। प्रसिद्ध विधिशास्त्री कार्वेट ने भी जोसेफ के इस सुझाव का समर्थन किया है।
प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :
(a) मान्यता की वापसी
(b) मान्यता का प्रतिवर्ती प्रभाव
(c) क्या मान्यता प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है
(d) मान्यता के परिणाम
(e) सशर्त मान्यता
Write shorts notes on the following:
(a) Withdrawal of Recognition
(b) Retrospective effects of Recognition
(c) Is Recognition a Duty of a states
(d) Consequences of Recognition
(c) Conditional Recognition
उत्तर- (a) मान्यता की वापसी (Withdrawal of Recognition)- इस प्रश्न पर विधिशास्त्रियों का विभिन्न मत है। इस प्रश्न का परीक्षण करने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्यता की वापसी का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य के विचार में अन्य राज्य अस्तित्व में नहीं रह गया है। मान्यता की वापसी का तात्पर्य राजनीतिक कारणों के लिए राज्य से वापसी हो सकती है किन्तु उसके अस्तित्व से नहीं। एक मत यह है कि वस्तुतः मान्यता प्रकृति में अस्थायी होने के कारण इसको उस समय वापस लिया जा सकता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मान्यता की आवश्यक शर्तों को पूरा किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। फ्रांस ने अक्टूबर, 1918 में उस वर्ष जनवरी में फिनिश गणतन्त्र की अस्थायी सरकार को प्रदान की गई मान्यता को वापस ले लिया था। इस मत के अनुसार विधितः मान्यता को वापस नहीं लिया जा सकता। इस मत का समर्थन 1933 मान्टेविडियों अभिसमय (Montevideo Convention) के अनुच्छेद 6 द्वारा किया गया है, जो घोषित करता है कि विधितः मान्यता बिना शर्त तथा अखण्डनीय होती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने सन् 1936 में स्वीकृत संकल्प में भी प्रावधान किया था कि एक बार दी गयी मान्यता वापस नहीं की जा सकती। दूसरा मत है कि मान्यता राजनीतिक कार्य है, इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं प्रतीत होता है कि क्यों मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, बशर्ते कि मान्यता प्रदान करने के कार्य के समान वह कार्य नीति का कार्य हो। यदि मान्यता प्रदान करने वाला राज्य यह समझता है कि राज्य ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी है, तो वह बाद वाले राज्य को प्रदत्त मान्यता को वापस ले सकता है। कभी-कभी मान्यता की वापसी मान्यता प्राप्त राज्य के प्राधिकारी की अभिव्यक्त अधिसूचना द्वारा या सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा की जाती है। लेकिन अभ्यास में, मान्यता की वापसी तब की जाती है जब इसकी वापसी के लिए अभिव्यक्त घोषणा हो और साथ ही साथ मान्यता वापस किये हुए राज्य के स्थान पर नये प्राधिकारी को मान्यता दी जा रही हो। यदि किसी राज्य का उपाबद्ध (annexation) के माध्यम से समापन हो जाता है और उस राज्य की सरकार का प्रशासन राज्य के बाहर से निर्वासित थोड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है, तब ऐसे अवसरों पर मान्यता की वापसी राज्य के राजनयिक प्रतिनिधियों की उस सूचना द्वारा उसी समय प्रभावी होती है कि उनके मिशन को समाप्त होना माना जाना चाहिए तथा वे अब से प्रश्नगत राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते रहेंगे।
यदि राज्य रजनीतिक आधारों पर राज्य की मान्यता को वापस लेना प्रारम्भ कर दें तो वे ऐसा करने के लिए कई अवसर पायेंगे। यदि यह अभ्यास उनके द्वारा प्रचलन में लाया जाता है तो स्थिति काफी अव्यवस्थित हो जायेगी। राज्यों का ऐसा कार्य राज्यों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रभावित करने के लिए सम्भाव्य है जिससे राज्यों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सहयोग प्रभावित हो सकता है। यह वांछनीय है कि राज्य एक बार प्रदान की गयी मान्यता को राजनीतिक सम्बन्धों से विच्छेद कर सकता है या कोई अन्य कदम उठा सकता है, किन्तु किसी भी मामले में मान्यता की वापंसी को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।
(b) मान्यता का प्रतिवर्ती प्रभाव (Retrospective Effects of Recognition)- मान्यता देने वाले राज्य नये राज्य में मान्यता प्राप्त होने के पहले के कार्य को वैध मान लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि साम्यवादी चीन को सन् 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता दी गयी थी, तो अमेरिका, साम्यवादी चीन के सभी कार्यों को उस तिथि से मानेगा, जब वह तथ्यतः अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश तथा अमेरिकी न्यायालय ने इस अभ्यास को अपनाया है। किन्तु उनके द्वारा अनुसरण किये जाने वाले अभ्यास को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। एक राज्य विधिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के उन कार्यों के लिए कैसे बाध्य होगा, जब उसके विचार में उसने राजत्व के आवश्यक गुणों को धारण ही नहीं किया था। यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो यह सुविधा के कारण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों एवं अनुकूल समझौता बनाये रखने के लिए या अपनी नीति के कारण। इस प्रकार मान्यता को प्रतिवर्ती प्रभाव देना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के किसी सिद्धान्त की अपेक्षा राष्ट्रीय नीति का मामला है। लेकिन उन मामलों में, जहाँ राज्य को पहले वस्तुतः मान्यता तथा बाद में विधितः मान्यता प्रदान की जाती है, वहाँ मान्यता का प्रभाव वस्तुतः मान्यता की तिथि से प्रारम्भ होता है। इसे प्रथम दृष्टि में नियम माना जाता है।
इस सम्बन्ध में सिविल एयर ट्रान्सपोर्ट इनकारपोरेटेड कम्पनी वनाम सेण्ट्रल एयरट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, (1953) एस० सी० 70 का मामला अच्छा उदाहरण है।
(c) क्या मान्यता प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है? (Is Recognition a Duty of a States)- इस मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों के मत भिन्न-भिन्न हैं। लाटर पैट (Lauter-pacht) का विचार है कि यदि एक बार राज्य राज्यत्व के सभी आवश्यक तत्वों को धारण कर लेता है तो नये राज्य को मान्यता प्रदान करना अन्य सभी राज्यों का कर्तव्य है। विद्यमान राज्यों का कर्त्तव्य मान्यता प्रदान करना है क्योंकि नये राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन विधिक अधिकार तथा कर्तव्य प्राप्त नहीं हो सकता यदि उसे राज्यों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। इनके अनुसार-
“राज्य के रूप में समुदाय को मान्यता प्रदान करना यह निश्चित करता है कि वह राज्यत्व की उन शर्तों को पूरा करता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अपेक्षित है। यदि ये तत्व विद्यमान हैं तो विद्यमान राज्य मान्यता प्रदान करने के कर्त्तव्य के अधीन हैं। पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की अपेक्षाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करने तथा प्रामाणिक रूप से घोषित करने के लिए सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय अंग के अभाव में पहले से स्थापित राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंग के रूप में अपनी सामर्थ्य में उस कृत्य को पूरा करते हैं। इस प्रकार कार्य करने में वे राष्ट्रों की विधि को लागू करते हैं।”
अतः लाटर पेट के अनुसार मान्यता देने वाले राज्य को इस बात से अवगत होना चाहिए कि वह नये राज्य को मान्यता देकर एक विधिक कार्य कर रहा है। कुछ लेखकों का मत है कि चूंकि नये राज्य को मान्यता देना एक विधिक कार्य है, यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सामूहिक रूप से सभी राज्यों को देना चाहिए। यह विधिक कृत्य राज्यों के ऊपर मनमाने ढंग से करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए।
किन्तु उपरोक्त मत मानने का तात्पर्य यह होगा कि नये राज्य को अधिकार है कि उसे अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दी जाये। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि नये राज्य के किसी ऐसे अधिकार के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं करती, इसलिए विद्यमान राज्यों का राज्य को मान्यता देने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं है। मान्यता प्रदान करना या मान्यता न देना विधि की अपेक्षा नीति का प्रश्न है इसलिए राज्य की मान्यता, राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करती है। स्वविवेक निर्णय एक राज्य का प्रभुत्व-सम्पन्न अधिकार है तथा इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यदि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों को विचार में लेने के बाद मान्यता के इस पहलू पर विचार किया जाता है तो निष्कर्ष दूसरा ही निकलता है। “राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना और विश्व शान्ति को सुदृढ़ करने के लिए अन्य समुचित उपाय करना, जो अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 2 के अधीन प्रावधानित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना जो अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 3 के अधीन प्रावधानित है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य है कि राज्य अन्य राज्यों को मान्यता नहीं प्रदान करते तो संयुक्त राष्ट्र के उक्त उद्देश्य के विफल हो जाने की सम्भावना है, क्योंकि बिना मान्यता प्राप्त राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना कठिन होता है और परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य नये राज्य को मान्यता देने के लिए विधिक कर्तव्य के अधीन हैं, यदि नया राज्य राजत्व के सभी आवश्यक गुणों को धारण कर लेता है।”
(d) मान्यता के परिणाम (Consequences of Recognition) – राज्य की मान्यता का दोहरा परिणाम होता है, अर्थात् राजनीतिक तथा विधिक। जहाँ तक राजनीतिक परिणाम का सम्बन्ध है, राज्य की मान्यता नये राज्य के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक क्रिया प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की इच्छा को दर्शित करता है। मान्यता विधितः सुसंगत है, क्योंकि यह प्रमाणित करती है कि मान्यता प्रदान करने वाला राज्य यह समझता है कि उसके मत में नई इकाई अन्तर्राष्ट्रीय विषय होने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करती है।
जब किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है, तब मान्यता प्रदान करने वाला राज्य उस राज्य के सम्बन्ध में कुछ अधिकारों को अर्जित करता है जो निम्नलिखित हैं-
(1) मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के साथ राजनयिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।
(2) मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के प्रतिनिधि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजनयिक उन्मुक्तियों के अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं।
(3) मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के साथ सन्धि- जात सम्बन्ध (Treaty Relationship) स्थापित कर सकते हैं। राज्यों द्वारा द्विपक्षीय सन्धि के निर्माण को एक-दूसरे के साथ उनके शासकीय मान्यता का साक्ष्य माना जाता है।
(4) मान्यता प्राप्त करने वाला मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालयों में वाद संस्थित करने के अधिकारों को प्राप्त कर लेता है।
(5) मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य मान्यता प्रदान करने वाले राज्य में स्थित सम्पत्ति का दावा कर सकता है।
उक्त परिणाम विद्यमान राज्यों को उतने राज्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, जितने को उसकी नीतियाँ मान्यता प्रदान करने के लिए अनुमति देती हैं। लेकिन यदि राज्य को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तो वह मान्यता के उक्त परिणामों का उपयोग नहीं कर सकता। अतः ये सभी मान्यता न देने की अयोग्यतायें (Disabilities of Recognition) कही जा सकती हैं। यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक को पूरा करने के लिए, अर्थात् “राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करने के लिए” जो चार्टर के अनुच्छेद 1 के परिच्छेद 2 में परिकल्पित है, मान्यता अधिक से अधिक राज्यों को प्रदान की जाये।
(e) सशर्त मान्यता (Conditional Recognition)- जब मान्यता प्रदान करने वाला राज्य राज्यत्व की सामान्य अपेक्षाओं के अलावा नये राज्य द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहता है, तो उसे सशर्त मान्यता कहते हैं। सशर्त मान्यता की अवधारणा को उस प्रोटोकाल में पेश किया गया था, जिस पर 28 जून, 1878 को सार्बिया की मान्यता के लिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी की ओर से हस्ताक्षर किया गया था। प्रोटोकाल में कहा गया था कि सर्विया को इस शर्त के अधीन मान्यता दी जा रही है कि वह अपने निवासियों पर कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा। सशर्त मान्यता देने वाला राज्य, मान्यता के एवज में अपने विशिष्ट लाभ के लिए शर्तें लगाता है। ओपेन हाइम ने उचित ही कहा है कि मान्यता विभिन्न पहलुओं में न तो संविधानात्मक प्रबन्ध है न ही राजनीतिक रियायत है। यह कतिपय तथ्यों की विद्यमानता की घोषणा है। ऐसा होने के कारण, इसे उन अपेक्षाओं, जो समुदाय को स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता के लिए अर्हित करता है, के लगातार अस्तित्व को शामिल करके अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य शर्तों के अध्यधीन करना अनुचित है। इस प्रकार, मान्यता प्रदान करते समय लगायी गयी शर्त मान्यता के वास्तविक कृत्य के प्रतिकूल होती है। राज्य की मान्यता सशर्त नहीं हो सकती है। यदि राज्य एक बार नये राज्य को मान्यता प्रदान कर देते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के विचार में, मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य राज्यत्व के सभी गुण धारण करता है। राज्यत्व के गुणों को धारण करने की मान्यता सशर्त नहीं हो सकती।
प्रश्न 11. अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं। स्पष्ट कीजिए।
How many territory come in State territory in International Law? Explain.
उत्तर- जिस क्षेत्र पर राज्य का नियन्त्रण एवं अधिकार होता है उसे राज्य का राज्यक्षेत्र कहा जाता है।
ओपेनहाइम के अनुसार, “क्षेत्र भूमण्डल (Globe) के उस निश्चित भाग को कहते हैं, जो राज्य के प्रभुत्व सम्पन्नता के अधीन होती है।” कार्फ् चैनल मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया था कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह जानबूझकर अन्य राज्यों के अधिकारों के प्रतिकूल कार्यों के लिए अपने राज्य क्षेत्र को प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा न दे। राज्य क्षेत्र में भू-राज्यक्षेत्र (Land Territory), राष्ट्रीय जल (National Water), राज्य क्षेत्रीय समुद्र (Territorial Sea), राज्यक्षेत्र के ऊपर वायुमण्डल (Air Space) तथा पृथ्वी के नीचे उप-भूमि (Sub-soil under-earth) शामिल रहती है।
(1) भू-राज्य क्षेत्र (Land Territory) राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत की उस राज्य का राज्यक्षेत्र होता है। सीमा पृथ्वी के सतह पर वह रेखा है जो एक राज्य के राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र से अलग करती है। राज्य क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए नदियाँ, चट्टानें या पहाड़ों की श्रेणी, रेगिस्तान या जंगल इत्यादि जैसी प्रकृतिक सीमाएँ होती हैं। दूसरी कृत्रिम सीमाएँ जो राज्यक्षेत्रों को विभाजित करने के प्रयोजन के लिए निर्मित को जाती हैं इसमें दीवार, स्तम्भ, खम्भा तथा खाईं (Trenches) इत्यादि शामिल हैं। चूंकि सीमा राज्यों के बीच विवाद का मुख्य स्रोत होता है इसलिए इसे हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि एक बार इसका निपटारा या तो सन्धि द्वारा या अधिकरण के पंचाट द्वारा कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से इस तथ्य की दृष्टि में इसमें व्यवधान नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि सीमा सन्धि सार्वभौमिक अधिकार (Right in Rem) को सृजित करती है।
(2) राष्ट्रीय जल (National Waters) राष्ट्रीय जल को आन्तरिक जल भी कहते हैं। यह नदियों, नहरों, झीलों (lakes) उपसागरों (Gulf) तथा खाड़ियों (Bays) को शामिल करता है।
(क) नदियाँ (Rivers)- नदियों को चार भागों में विभाजित किया जाता है- पहले प्रकार की नदियाँ उद्गम स्थल से मुहाने तक बहती हैं। दूसरी वे नदियाँ जो दो भिन्न राज्यों को एक-दूसरे से अलग करती हैं, तीसरी वे नदियाँ हैं जो कई राज्यों से होकर बहती हैं इन्हें गैर-राष्ट्रीय नदियों के रूप में भी जाना जाता है। चौथी वे नदियाँ हैं जो खुले समुद्र के नौगम्य (Navigable) होती हैं
(ख) नहर (Canals)- नहरों का निर्माण राज्यों द्वारा किया जाता है। ये अधिकतम सम्बन्धित राज्यों के राज्य क्षेत्रों का भाग होती हैं। किन्तु कभी-कभी जब ये इस तरह से निर्मित की जाती हैं जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग व्यवस्था (International Waer-way System) या अन्तर्राष्ट्रीय जल निकासी व्यवस्था (International Drainage System) प्रभावित हो जाते हैं तब तो वे अन्य राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हें अन्तर- महासागरीय नगरों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। स्वेज नहर (Suez Canal) कील नहर (Kiel Canal), पनामा नहर (Panama Canal) तथा डार्डेनल्स ऐसी नहरों के उदाहरण है।
अन्य राज्यों द्वारा नहर का प्रयोग तथा राज्य क्षेत्रीय राज्य का नियन्त्रण सन्धियों द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण नहरें निम्नलिखित हैं-
(i) स्वेज नहर (Suez Canal)
(ii) कौल नहर (Kiel Canal)
(iii) पनामा नहर (Panama Canal) |
(ग) जल संयोजी (Straits)- जो जल संयोजी एक तथा उसी राज्य की भूमि को विभाजित करते हैं, वे उस राज्य से सम्बन्धित होते हैं जो जल संयोजी छह मील से अधिक चौड़े होते हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जल संयोजी (International Straits) कहा जाता है। यह विवाद का प्रश्न है कि वे तटवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र हैं या नहीं।
कार्फ् चैनेल वाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि निर्दोष यात्रा का प्रयोग तटवर्ती राज्यों के पूर्व प्राधिकार के बिना किया जा सकता है।
वर्तमान में, जल संयोजी से सम्बन्धित विधि को संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982) द्वारा संहिताबद्ध कर दिया गया है। अभिसमय के अनुच्छेद 34 का परिच्छेद 1 प्रावधान करता है कि इस भाग में प्रतिपादित नौकाचालन के लिए प्रयुक्त जल संयोजी के माध्यम से यात्रा नियम (Regime of Passage) अन्य सम्बन्धों में ऐसे जल संयोजी को गठित करने वाले जल की विधिक प्रास्थिति तथा जल संयोजी के तटवर्ती राज्यों द्वारा ऐसे जल तथा उनके वायुमण्डल, तल (bed) या उप-भूमि (Sub-soil) पर उनकी प्रभुत्व सम्पन्नता या अधिकारिता के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा।
(घ) खाड़ी (Bays) समुद्र विधि अभिसमय, 1982 अनुच्छेद 10 (2) के अधीन “खाड़ी” को सुचिह्नित (Well Marked), गड्डा (Indentation) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका व्यापन (Penetration) इसके मुहाने (Mouth) की चौड़ाई के ऐसे अनुपात में है, जो भू-बद्ध (Land Locked) जल को अन्तर्विष्ट करे तथा तट में केवल एक मोड़ से अधिक मोड़ बनायें।
माप के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 10 परिच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि गड्डा का क्षेत्र गड्डा के किनारे चारों तरफ कम जल चिह्न तथा इसके प्राकृतिक प्रवेश बिन्दु के कम जल चिह्न को जोड़ने वाली रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र है।
अनुच्छेद 10 का परिच्छेद 5 प्रावधान करता है कि जहां खाड़ी के प्राकृतिक प्रवेश बिन्दु के पिछले जल चिह्न के मध्य दूरी 24 समुद्री मील आधार रेखा खाड़ी के अन्तर्गत इस ढंग में खींची जायेगी, जो जल के अधिकतम क्षेत्र को परिबद्ध करे जो उस लम्बाई की रेखा के साथ सम्भव हो। यह प्रावधान तथाकथित ‘ऐतिहासिक’ खाड़ियों या किसी ऐसे मामलों में लागू नहीं होते जहां अनुच्छेद 7 में प्रवधानित सीधी आधार रेखा की प्रणाली लागू होती है। इस प्रकार राज्य ऐतिहासिक हक के अधीन खाड़ियों में प्रभुत्व सम्पन्नता का दावा कर सकते हैं।
(ङ) झील तथा भू-बद्ध समुद्र (Lakes and land Locked Seas) ओपेनहाइम के अनुसार, “उन झीलों तथा अन्तर्देशीय समुद्रों के लिए जिसके एक से अधिक तटीय राज्य होते हैं, वे सामान्यतया जलों को विभाजित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्थापित करती हैं और इसमें भूमि सीमा से सम्बन्धित विधि लागू होगी।”
पेरिस शान्ति सन्धि, 1956 (Peace Treaty of Paris, 1856) के अनुच्छेद 11 में काला सागर को तटस्थ क्षेत्र बता दिया और इसे सभी राष्ट्रों के व्यापारियों के लिए खुला घोषित किया। लन्दन सम्मेलन में 13 मार्च, 1871 को लन्दन सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें काला सागर के तटस्थीकरण का उन्मूलन कर दिया गया लेकिन काला सागर पर सभी राष्ट्रों के व्यापारियों के लिए स्वतन्त्र-नौ संचालन का अनुमोदन किया गया।
इस प्रकार काला सागर खुला समुद्र है किन्तु गैर-तटीय राज्यों के लिए उसमें पहुँच सीमित है।
इसके अलावा राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रीय समुद्र (Territorial Sea) भी आता है। राज्य क्षेत्रीय समुद्र को कभी-कभी राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड (Territorial Waters) भी कहा जाता है। हेग संहिताकरण सम्मेलन, 1930 में ‘राज्यक्षेत्रीय समुद्र’ शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य क्षेत्रीय समुद्र को उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी राज्य के तट से संलग्न है तथा जिस पर तटवर्ती राज्यों की प्रभुत्व सम्पन्नता होती है। राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा संलग्न क्षेत्र जेनेवा अभिसमय, 1958 में अभिव्यक्त रूप से अनुच्छेद 1 के अधीन राज्य क्षेत्रीय समुद्र पर तटवर्ती राज्यों की प्रभुत्व सम्पन्नता इसके भू-राज्यक्षेत्र तथा इसके आन्तरिक जल के परे इसके तट से संलग्न समुद्र की पेटी तक विस्तारित है, जिसे राज्य क्षेत्रीय समुद्र कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत वायुमण्डल (Air-space) एवं जमीन के नीचे की उप-भूमि (Sub-soil under earth) भी आती है।
प्रश्न 12 अन्तर्राष्ट्रीय विधि में समुद्र विधि का विकास कैसे हुआ? समुद्र विधि में अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें।
How developed the Law of the Sea in International Law? What do you understand by exclusive economic zone in the law of Sea? Explain.
उत्तर- समुद्र-विधि का विकास ग्रोशियस (Grotius) के समय में हुआ तथा राज्यों द्वारा इनका अनुपालन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रूढ़िगत नियमों के रूप में किया जाता था। सम्पूर्ण समुद्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता था। प्रथम, राज्य क्षेत्रीय समुद्र (Territorial Sea) दूसरा संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) तथा तीसरा खुला समुद्र। इनसे सम्बन्धित विधियाँ उन्नीसवीं शताब्दी तक निश्चित हो गयी थीं। लेकिन वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से कुछ ऐसे विकास होने लगे जिससे समुद्र विधि पर फिर से विधि बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी।
हेग संहिताकरण सम्मेलन (Hagues Codification Conference) ने 1930 में, समुद्र-विधि के कुछ पहलुओं को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया किन्तु इसका प्रयास व्यर्थ हो गया। आर्थिक तथा सैनिक हित ने कुछ राज्यों को 200 मील तक राज्यक्षेत्रीय समद्र की चौड़ाई का दावा करने के लिए प्रेरित किया। इन दावों ने गम्भीर समस्याओं को उत्पन्न किया।
प्रथम व द्वितीय संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन (First and Second U.N. Conference on the Law of the Sea) – इस सम्मेलन में 82 राज्य उपस्थित थे। जेनेवा सम्मेलन में 4 अभिसमयों को अंगीकृत किया गया। राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा संलग्न क्षेत्र अभिसमय, खुला समुद्र अभिसमय मछली पकड़ने तथा जीवित स्रोतों का संरक्षण अभिसमय तथा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि अभिसमय (Convention on the Continental Shelf)। उपरोक्त सभी अभिसमय लागू हो गये। इस सम्मेलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण विवाद जो बिना निर्णय किए छोड़ दिया गया था, वह था राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी राज्य इस क्षेत्र की एक सीमा पर सहमत नहीं थे। इसके उपरान्त खनिज स्रोतों का सर्वेक्षण माल्टा के प्रतिनिधि अर्वोड पार्डों द्वारा किया गया।
तीसरा संयुक्त राष्ट्र विधि सम्मेलन (Third U.N. Conference on the Law of the Sea) खनिजों की आवश्यकता और अन्य कारणों जैसे सैनिक और सामरिक पहलुओं ने ऐसी विधि के निर्माण को अनिवार्य बना दिया, जो सम्भवतः अत्यधिक प्रभावी ढंग से समुद्र को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सके। इसलिए 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने तीसरा संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन का प्रथम सत्र 1973 में न्यूयार्क में आयोजित किया गया।
समुद्र विधि अभिसमय, 1982 (Convention on the Law of the Sea, 1982) सम्मेलन के ग्यारहवें सत्र में 30 अप्रैल, 1982 को 130 राज्यों के भारी बहुमत से समुद्र-विधि अभिसमय के प्ररूप को स्वीकृत किया गया। इसमें यह भी निश्चित किया गया कि अभिसमय पर 10 दिसम्बर, 1982 को जमैका में हस्ताक्षर किया जायेगा। उस दिन 117 राज्यों ने अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। लेकिन अभिसमय हस्ताक्षर के लिए 9 दिसम्बर, 1984 तक खुला रहा।
समुद्र विधि अभिसमय, 1982 में 320 अनुच्छेद हैं। इन्हें 17 भागों तथा 9 परिशिष्टों में विभाजित किया गया है। अभिसमय 60 राज्यों द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किये जाने के 12 मास बाद लागू हुआ। अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाला पहला राज्य जमेका था और अनुसमर्थन का 60वां दस्तावेज गुयाना द्वारा 16 नवम्बर, 1993 को जमा किया गया। अतः अभिसमय 16 नवम्बर, 1994 को लागू हुआ। अभिसमय के दिसम्बर, 2002 तक 141 राज्य पक्षकार बन चुके हैं जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि अभिसमय के भाग 11 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित करार, 1994 (Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1994)- जुलाई 1990 के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूलर ने औपचारिक विचार-विमर्श आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अभिसमय में सार्वभौमिक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह उल्लेख किया कि अभिसमय को अंगीकृत किये जाने के बाद आठ वर्षों में कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन हुये हैं, जिनका अभिसमय में अन्तर्विष्ट गहरे समुद्र तल के खनन की व्यवस्था पर सुस्पष्ट प्रभाव पड़ा है। महासचिव के तत्वाधान में अनौपचारिक विचार-विमर्श वर्ष 1990 से 1994 के बीच किये गये जिसके दौरान 15 बैठकें आयोजित की गयीं। अनौपचारिक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप महासभा द्वारा 1982 के अभिसमय के गहरे समुद्र तल के खनन के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर करार को अंगीकार किया गया।
करार के प्रावधानों तथा अभिसमय के भाग 11 का निर्वचन एक दस्तावेज (Single Instrument) के रूप में किया जायेगा और इन्हें एक दस्तावेज के रूप में लागू किया जायेगा। दोनों के बीच किसी असंगति की स्थिति में, करार के प्रावधान अभिभावी होंगे। जो संलग्नक (Annexure) में अधिकधित किये गये हैं और जो करार के अभिन्न भाग हैं।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में समुद्र विधि तृतीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में पूर्ण रूप से विचार-विमर्श तथा विचारण किया गया। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को अन्तिम रूप से समुद्र विधि अभिसमय, 1982 में स्थान मिला। तभी से यह सामान्य रूप से समुद्र विधि का एक स्वीकृत भाग हो गया है। ट्यूनीशिया बनाम लीबिया के बाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र को रूढ़िगत नियमों का भाग कहा जा सकता है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा – अनन्य आर्थिक क्षेत्र राज्य क्षेत्रीय समुद्र के परे तथा उससे संलग्न वह क्षेत्र है, जिसका विस्तार 200 समुद्री मील तक होता है। इसकी माप वहीं से होगी जहाँ से राज्य क्षेत्रीय समुद्र को माप होती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बाह्य सीमा मापक्रम (Scale) के चार्ट में दर्शित की जायेगी जिसको तटवर्ती राज्य प्रकाशित करेंगे। जहाँ तक चौड़ाई का सम्बन्ध है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के बीच अन्तर है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की चौड़ाई की सीमातट रेखा से 200 समुद्री मील तक ही होगी, जबकि महाद्वीपीय मग्नतट भूमि की चौड़ाई अनन्य आर्थिक क्षेत्र को शामिल कर लेती है। इसका अर्थ यह होता है कि महाद्वीपीय मग्नतट भूमि वहाँ से हो सकती है, जहाँ अनन्य आर्थिक क्षेत्र नहीं है किन्तु समवर्ती महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के बिना अनन्य आर्थिक क्षेत्र नहीं हो सकता। इस प्रकार दो संस्थान महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधुनिक विधि में एक साथ सम्बद्ध हैं।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तटवर्ती राज्यों के अधिकार – अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तटवर्ती राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों, समुद्र तथा इसके उपभूमि के उपरिवर्ती जल के जीवित तथा अजीवित संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन संरक्षण तथा प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए ‘प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार’ है। तटवर्ती राज्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र ऊपर उक्त प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र का समीकरण राज्य क्षेत्रीय समुद्र के साथ नहीं किया जा सकता, जिसे राज्यक्षेत्र का भाग माना जाता है तथा जिस पर राज्यों की प्रभुत्व सम्पन्नता रहती है। इस प्रकार अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विनियोजन नहीं किया जा सकता। “प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार” शब्द संज्ञापित करता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का प्रयोग केवल तटवर्ती राज्यों के इसके तटवर्ती सागर खण्ड में अन्तर्विष्ट संसाधनों पर उसके अधिकारों की अनन्यता के अर्थ में किया जा सकता है। जब तक वे स्वयं इस क्षेत्र को दूसरे राज्य को नहीं दे देते तब तक उन अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता।
तटवर्ती राज्य क्षेत्र इस क्षेत्र में जीवित संसाधनों के अन्वेषण, दोहन, संरक्षण तथा प्रबन्ध करने के अपने प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में विधि तथा विनियम बना सकते हैं। यह शर्तों तथा निबन्धनों (Terms) को निर्धारित करते हए कई विनियम पारित कर सकते हैं, जिनका अनुपालन अन्य राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन विनियमों से अभिसमय के अनुरूप होने की अपेक्षा की जाती है। उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य नियन्त्रण, निरीक्षण, गिरफ्तारी तथा न्यायिक कार्यवाही को शामिल करके ऐसे उपाय कर सकते हैं जो विधियों तथा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। विदेशी जलयानों की गिरफ्तारी या निरोध के मामले में तत्परता से ध्वज राज्य को अधिसूचित करना तटवर्ती राज्य का कर्तव्य है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकार- 1982 के अभिसमय का अनुच्छेद 54 का परिच्छेद 2 स्पष्ट रूप से अधिकधित करता है कि तटवर्ती राज्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रयोग में अन्य राज्यों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का सम्यक् ध्यान रखेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अभिसमय के अनुच्छेद 58 के अधीन भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 58 के परिच्छेद 3 के अधीन अन्य राज्यों के अधिकारों पर सामान्य प्रतिबन्ध अधिरोपित किये गये हैं। इसके अनुसार सभी राज्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रयोग में तथा अपने कर्तव्यों के पालन में तटवर्ती राज्य के अधिकारों तथा कर्तव्यों का सम्यक् ध्यान रखेंगे। अन्य राज्य भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान संचालित कर सकते हैं लेकिन इसे केवल तटवर्ती राज्यों की सम्मति से तथा केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही संचालित किया जा सकता है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र की प्रास्थिति चूँकि तटवर्ती राज्य को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर “प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार” दिया गया है, इसलिए इस क्षेत्र की प्रकृति तथा प्रास्थिति में पूर्णतया परिवर्तन हो गया है। यह क्षेत्र खुले समुद्र का भाग नहीं रह गया है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा उस समय से आरम्भ हुई जब 1982 का समुद्र विधि अभिसमय 16 नवम्बर, 1994 से लागू हुआ। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अभिसमय के लागू होने से पहले ही 112 राज्यों ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता को अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग कर लिया था। इससे यह आशय निकलता है कि यदि अभिसमय लागू न भी होता फिर भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित प्रावधान राज्यों के अभ्यास के आधार पर सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भाग बन जाता।
सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अधीन प्रावधान करता है कि “भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र राज्यक्षेत्रीय समुद्र से संलग्न तथा उसके परे है, तथा ऐसे क्षेत्र की सीमा इस आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है जहाँ से राज्यक्षेत्रीय समुद्र की माप की जाती है।”
प्रश्न 13. समुद्र-विधि में खुला समुद्र से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
What do you understand by High Seas in the Law of Sea. Explain.
उत्तर- खुला समुद्र (High Seas)- “खुला समुद्र” शब्द से तात्पर्य समुद्र के उस भाग से है, जो राज्य क्षेत्रीय समुद्र में शामिल नहीं किये जाते हैं। इस नियम को 17वीं शताब्दी में योशियस द्वारा अपनी पुस्तक मारे लिब्रम (Mare Libram) में बताया गया था। बाद में 18वीं शती के प्रसिद्ध न्यायविदों ने भी खुले समुद्र की स्वतन्त्रता का समर्थन किया, जिनमें बार्यकर शाक प्रमुख थे। 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश के अंत तक खुले समुद्र की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को सार्वभौमिक रूप से सिद्धान्त तथा अभ्यास में मान्यता दी गयी। इस नियम को 1958 में खुला समुद्र जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention on Seas) को अंगीकार कर सन्धिगत विधि में परिवर्तित कर दिया गया था। अभिसमय का अनुच्छेद 1 ‘खुला समुद्र’ को परिभाषित करता है जिसके अनुसार, “खुला समुद्र, समुद्र जो राज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में या राष्ट्रीय जल में शामिल का यह भाग है नहीं है लेकिन खुले समुद्र की व्यवस्था को समुद्र विधि अभिसमय, 1982 के अधीन व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। अनुच्छेद 86 यह प्रावधान करता है कि समुद्र के वे सभी भाग खुले समुद्र के अधीन आयेंगे, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में राज्यक्षेत्रीय समुद्र में या राष्ट्रीय जल में या द्वीप समूहित राज्य के द्वीप समूहित सागर खण्ड में शामिल नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार खुले समुद्र का क्षेत्र 1982 के अभिसमय के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से कम हो गया है।
खुले समुद्र की स्वतन्त्रतायें (Freedoms of the High Seas) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रूढ़िगत नियम के अधीन खुला समुद्र सभी राज्यों के लिए स्वतन्त्र तथा खुला था। “खुले समुद्र की स्वतन्त्रता” एक मान्यता प्राप्त सिद्धान्त था। इस नियम के अनुसार राज्यों को खुले समुद्र में नौकाचालन तथा मछली उद्योग की स्वतन्त्रता थी। अतः खुला समुद्र सभी राज्यों के लिए समान था, जिससे कोई राज्य उसके किसी भाग को अपनी राज्यक्षेत्रीय प्रभुत्व सम्पन्नता का विषय नहीं बन सकता था। चूँकि खुला समुद्र किसी राज्य का राज्यक्षेत्र नहीं है इसलिए किसी राज्य को नियमतः खुले समुद्र के भाग पर अपने विधायन, प्रशासन, अधिकारिता या पुलिस का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। चूँकि खुला समुद्र किसी राज्य की प्रभुत्व सम्पन्नता के अधीन कभी नहीं हो सकता, इसलिए किसी राज्य को अधिभोग (Occupation) के माध्यम से खुला समुद्र से किसी भाग को अर्जित करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि खुला समुद्र किसी राज्य का राज्यक्षेत्र नहीं हो सकता फिर भी इस क्षेत्र के लिए विधि निर्मित की गयी है। राष्ट्रों के विधि के निम्नलिखित नियमों को सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गयी है-प्रथम प्रत्येक राज्य, जिसके पास सामुद्रिक ध्वज है, को ऐसा नियम प्रतिपादित करना चाहिए, जिसके अनुसार जलयान उसके ध्वज के अधीन जलयात्रा करने का दावा कर सकते हैं और ऐसे जलयानों को अपना ध्वज प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुये कुछ शासकीय बाउचर प्रदान करना चाहिए। दूसरा प्रत्येक राज्य को ऐसे सभी विदेशी जलयानों को दण्डित करने का अधिकार है, जो ऐसा करने के लिए प्राधिकार प्राप्त किये बिना उसके ध्वज के अधीन जलयात्रा करते हैं। तीसरा सभी जलयान अपने व्यक्तियों तथा मालों के साथ जब खुले समुद्र पर हो, ध्वज राष्ट्र के मार्ग में माने जाते हैं, चौथा, प्रत्येक राज्य को जलदस्युता को दण्डित करने का अधिकार है, भले ही वह विदेशियों द्वारा कारित किया गया हो।
समुद्र विधि अभिसमय, 1982 ने अनुच्छेद 87 के अधीन प्रावधान किया है कि खुला समुद्र सभी राज्यों के लिए खुला है, चाहे वे तटवर्ती राज्य हों या भू-बद्ध। लेकिन इसकी स्वतन्त्रता का प्रयोग इस अभिसमय द्वारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य नियमों द्वारा कथित शर्तों के अधीन किया जायेगा। अभिसमय के अधीन खुले समुद्र की स्वतन्त्रता नौपरिवहन की स्वतन्त्रता, ऊपरी उड़ान की स्वतन्त्रता, अन्तः समुद्री तारों तथा नल-यन्त्रों को फैलाने की स्वतन्त्रता, कृत्रिम द्वीपों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि अनुज्ञात, अन्य संस्थापनाओं को सन्निर्मित करने की स्वतन्त्रता, मछली मारने की स्वतन्त्रता, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतन्त्रता को शामिल करता है। इन स्वतन्त्रताओं का प्रयोग सभी राज्यों द्वारा खुले समुद्र की अपने स्वतन्त्रताओं के प्रयोग में अन्य राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए किया जायेगा।
खुले समुद्र की स्वतन्त्रता पर परिसीमा (Limitations on the Freedom of the High Sea)- अभिसमय 1982 का अनुच्छेद 87 (2) खुले समुद्र की स्वतन्त्रता पर सामान्य प्रकृति की परिसीमा यह अधिकथित करते हुये अधिरोपित करता है कि खुले समुद्र की स्वतन्त्रता का प्रयोग अन्य राज्यों के हितों को सम्यक् ध्यान में रखकर किया जायेगा। इस सामान्य परिसीमा के अतिरिक्त समुद्र की स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के अधिकार पर निम्नलिखित अन्य परिसीमायें हैं-
(1) मछली मारने की स्वतन्त्रता (Freedom of Fishing)- सभी राज्यों को खुले समुद्र पर मछली मारने की स्वतन्त्रता है किन्तु अभिसमय, 1982 का अनुच्छेद 117 अधिकथित करता है कि सभी राज्यों को खुले समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए ऐसा उपाय करने या अन्य राज्यों द्वारा ऐसा उपाय करने में सहयोग करने का कर्त्तव्य है।
(2) नौसंचालन की स्वतन्त्रता (Freedom of Navigation) अभिसमय, 1982 का अनुच्छेद 94 सारभूत न्यूनतम अपेक्षाओं को अभिकथित करता है, जिनका अनुपालन सभी राज्यों को नौसंचालन की सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेषकर जलयानों के सन्निर्माण, साज-सज्जा समुद्र योग्यता तथा संचालन जलयान पर श्रमिकों की स्थिति, अधिकारों के प्रयोग, संसूचना का रख-रखाव तथा टक्कर की निवारण के सम्बन्ध में किया जाना चाहिए।
(3) वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतन्त्रता (Freedom of Scientific Research)- अभिसमय, 1982 का अनुच्छेद 261 वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतन्त्रता पर नौसंचालन की स्वतन्त्रता के प्रयोग को अधिमानता देता है, यह अधिमानता केवल स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय जलयान मार्ग में वैज्ञानिक संस्थापन और उपकरण के प्रयोजन के सम्बन्ध में ही है।
(4) युद्धपोतों से हस्तक्षेप नहीं करना (Non-interference with the Warships) अनुच्छेद 95 प्रावधान करता है कि खुले समुद्र पर युद्धपोतों को ध्वजवाहक राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों की अधिकारिता से पूर्ण उन्मुक्ति है। अभिसमय, 1982 के अनुच्छेद 110 के अधीन उपबन्ध किया गया है, जिसमें जलयान पर जाने का अधिकार शामिल है, जब इस सन्देह के लिए युक्तियुक्त आधार है कि जलयान जल-दस्युता में संलग्न है या जलयान अप्राधिकृत प्रसारण में संलग्न है, जलयान बिना राष्ट्रीयता के है या यद्यपि विदेशी ध्वज लहराते हुये या अपना ध्वज दर्शित करने से इन्कार करते हुये, जलयान वास्तव में उसी राष्ट्रीयता का है, जिसका युद्धपोत है।
(5) क्षेत्र में क्रियाकलाप (Activities in the Area) अभिसमय, 1982 के अनुच्छेद 87 का परिच्छेद अधिकथित करता है कि खुले समुद्र की स्वतन्त्रता का प्रयोग सभी राज्यों द्वारा क्षेत्र में क्रियाकलाप के सम्बन्ध में अभिसमय के अधीन अधिकारों को ध्यान में रखकर किया जायेगा। इस प्रकार राज्यों को इस सम्बन्ध में स्वयं समायोजन करना है।
प्रश्न 14. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
(1) राज्य क्षेत्रीय समुद्र
(2) संलग्न क्षेत्र
(3) वायु-क्षेत्र
(4) अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ
(5) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण
Write short notes on following:
(1) Territorial Sea
(2) Contiguous Zone
(3) Air Space
(4) International Rivers
(5) International Sea-bed Authority.
उत्तर- (1) राज्यक्षेत्रीय समुद्र (Territorial Sea)- हेग संहिताकरण सम्मेलन, 1930 (The Hague Codification Conference of 1930) में “राज्यक्षेत्रीय समुद्र” शब्द का प्रयोग किया गया है। जेनेवा सम्मेलन, 1958 के समय से हो सामान्य ‘राज्यक्षेत्रीय समुद्र’ शब्द का प्रयोग किया गया है। समुद्र विधि अभिसमय, 1982 में राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड’ की अपेक्षा ‘राज्य क्षेत्रीय समुद्र’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ओपेनहाइम के अनुसार राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड शब्द का प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि कभी-कभी इसका प्रयोग आन्तरिक जलों को निर्दिष्ट करने तथा कभी-कभी आन्तरिक जल तथा राज्यक्षेत्रीय समुद्र को संयुक्त रूप से निर्दिष्ट करने के लिए भी किया जाता है।
राज्य की प्रभुत्व-सम्पन्नता न केवल इसकी सीमाओं के अन्तर्गत स्थित जल तथा भूमि तक सीमित है बल्कि यह समुद्र के उस भाग तक भी विस्तारित है, जो तटवर्ती राज्य से संलग्न है। यह जल निश्चित क्षेत्र (Zone) या पेटी (Belt) में समाहित रहता है, जिसे “सीमान्त क्षेत्र” (Marginal Zone) या “सीमान्त पेटी (Marginal Belt) कहा जाता है।
राज्यक्षेत्रीय समुद्र की अवधारणा में दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। ये हैं- राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई तथा उस पर राज्यों का अधिकार।
(2) संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) – तटवर्ती राज्यों की पुलिस तथा राजस्व अधिकारिता का विस्तार संलग्न क्षेत्र तक है। संलग्न क्षेत्र जेनेवा अभिसमय, 1958 ने अनुच्छेद 24 परिच्छेद 1 के अधीन तटवर्ती राज्यों के अधिकार को मान्यता दी है। इसके अनुसार “तटवर्ती राज्य (क) अपने राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय समूह के अन्तर्गत अपने सीमा शुल्क, वित्तीय अप्रवासन या सफाई विनियमों के उल्लंघन को रोकने, (ख) राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के अन्तर्गत उक्त विनियमों के उल्लंघन को दण्डित करने के लिए आवश्यक नियन्त्रण का प्रयोग कर सकते हैं।” इसी तरह का प्रावधान 1982 के अभिसमय के अनुच्छेद 33 के अधीन भी किया गया है।
संलग्न क्षेत्र की सीमा के सम्बन्ध में 1958 के जेनेवा अभिसमय में प्रावधान किया गया है। इसका विस्तार उस आधार रेखा से 12 मील तक है, जिससे राज्यक्षेत्रीय समुद्र की माप की जाती है। इस प्रकार संलग्न क्षेत्र की अवधारणा उन राज्यों के लिए अर्थहीन थी, जिन्होंने 12 मील तक राज्यक्षेत्रीय समुद्र का दावा किया था। उन्होंने संलग्न क्षेत्र की सीमा की राज्यक्षेत्रीय समुद्र में शामिल कर दिया है। संलग्न क्षेत्र की सीमा का विस्तार 1982 के अभिसमय द्वारा किया गया है, जो अनुच्छेद 33 परिच्छेद 2 के अधीन प्रावधान करता है कि इसका विस्तार उस आधार रेखा से 24 समुद्री मील के आगे नहीं हो सकता, जिसमें राज्य क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई की माप की जाती है।
चौंक समुद्र विधि अभिसमय, 1982 में अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा विकसित की गयी है. इसलिए संलग्न क्षेत्र को अब और अधिक समय तक खुला समुद्र का भाग नहीं माना जायेगा। चूँकि अनुच्छेद 33 आज्ञापक है और बैंक संलग्न क्षेत्र जहाँ ऐसे क्षेत्र का दावा किया जाता है पूर्णतया अनन्य आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र में होते हैं, इसलिए शायद यह संदेहास्पद है कि क्या किसी राज्य को संलग्न क्षेत्र की अधिकारिता के सम्बन्ध में औपचारिक रूप से संलग्न क्षेत्र का दावा करने या घोषणा करने की आवश्यकता है।
संलग्न क्षेत्र पर भारतीय स्थिति (Indian Position on Contiguous Zone)- भारत में सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 को अधिनियमित करके 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र का दावा किया गया है। अधिनियम की धारा 5 प्रावधान करती है कि भारत का संलग्न क्षेत्र राज्य क्षेत्रीय समुद्र के परे तथा उससे संलग्न क्षेत्र है तथा क्षेत्र का विस्तार उस रेखा तक है, जो तट से 24 समुद्री मील की दूरी पर है।
(3) वायु-क्षेत्र (Air Space)- प्रत्येक राष्ट्र अपने सीमा क्षेत्र पर सम्पूर्ण सम्प्रभुत्व (Sovereignty) रखता है। सीमा क्षेत्र में भूमि, जल, समुद्री तट तथा वायु स्थान (Air Space) भी सम्मिलित है। प्राचीन विचारधारा के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को उसके सम्पूर्ण वायुक्षेत्र (आकाश) पर सम्प्रभुत्व प्राप्त थी परन्तु आधुनिक विचारधारा में इस मान्यता की आलोचना की गयी तथा विधि विशेषज्ञों ने प्राचीन विचारधारा की आलोचना की। इस विषय में कई विचारधारा तथा सिद्धान्त प्रचलित हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार वायु स्थान (Air Space) प्रत्येक राष्ट्र को प्राप्त है तथा प्रत्येक राष्ट्र के वायुयान इस वायु स्थान (Air Space) से बिना किसी रोक-टोक आ-जा सकते हैं। इस विचारधारा की प्रचण्ड आलोचना हुई क्योंकि यह कई अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के प्रतिकूल थी। प्रत्येक राष्ट्र को अपने क्षेत्र के वायुस्थान पर नियन्त्रण करने का अधिकार है तथा दूसरे राष्ट्र का वायुयान किसी राष्ट्र के वायु स्थान (Air Space) में उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करके ही प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने वायुस्थान (Air Space) पर असीमित ऊँचाई (Unlimited Height) तक नियन्त्रण प्राप्त है। उसे इस क्षेत्र पर पूर्ण नियन् प्राप्त है तथा उस क्षेत्र में दूसरे राष्ट्र के वायुयान को प्रवेश की अनुमति न देने का यह राष्ट्र अधिकार रखता है। यह विचारधारा भी सही नहीं थी क्योंकि त्वरित तकनीकी तथा वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा निर्मित वायुयान बहुत अधिक ऊँचाई तक जा सकते हैं तथा प्रत्येक राष्ट्र के लिए इतनी अधिक ऊँचाई तक नियन्त्रण कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिए इस विचारधारा ने अपना महत्व खो दिया। दोसरी विचारधारा के अनुसार एक राष्ट्र को अपने वायुयान (आकाश के निचले सार) पर ही नियन्त्रण प्राप्त है तथा इसकी सम्प्रभुता इसी स्तर तक ही सीमित है। यह विचारधारा पूर्व उल्लिखित अन्य दो विचारधारों से अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है क्योंकि सम्प्रभुता तभी प्रभावी होगी जब उस पर राष्ट्र नियन्त्रण कर सके। परन्तु इस सिद्धान्त को स्वीकारने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कोई भी राष्ट्र इस सिद्धान्त पर सहमत होने को तैयार नहीं है। चौथी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि बाह्य स्थल (Outer Space) की सुरक्षा सुनिश्चित करने सम्बन्धी नियम बनाये। परन्तु विश्व के बहुत कम राष्ट्र इस नियम का पालन सुनिश्चित करवा सकते हैं। अन्त में प्रत्येक राष्ट्र को अपने वायु क्षेत्र पर असीमित ऊँचाई तक सम्प्रभुता प्राप्त है। परन्तु दूसरे राष्ट्र के वायुयानों का निर्दोष प्रवेश इस नियम के अन्तर्गत नहीं होगा।
इस प्रकार वायु क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। परन्तु कुछ बातों पर आम सहमति है जैसे (1) प्रत्येक राष्ट्र को अपने वायुक्षेत्र पर नियन्त्रण प्राप्त है जो उसकी सीमा में है परन्तु उसी समय व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा मानवतावादी उद्देश्यों के लिए वायु आवागमन की भी आवश्यकता है। इस परस्पर विरोधी आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करने हेतु कामचलाऊ सम्प्रभुता का सुझाव दिया गया। वायु क्षेत्र के प्रशासन में विधिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि की नवीन शाखा का सृजन आवश्यक है। नवम्बर, 1944 में शिकागों में अन्तर्राष्ट्रीय उड्डूयन सम्मेलन में वायु स्वतन्त्रता के लिये पाँच स्वतन्त्रताओं पर सहमति हुई-
(1) बिना उत्तरे विदेशी सीमा क्षेत्र पर उड़ने की स्वतन्त्रता;
(2) बिना यातायात के उद्देश्य के भूमि पर उतरने की स्वतन्त्रता;
(3) मूल वायुयान के राष्ट्र से उद्भूत वायुयान में विदेशी भूमि पर मार्ग समाप्ति का अधिकार;
(4) वायुयान के मूल राष्ट्र के यात्रियों को विदेशी भूमि से उठा लेने का अधिकारः
(5) दो विदेशी राष्ट्रों के मध्य यातायात जारी रखने का अधिकार।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ (International Rivers)- नदियों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-
(1) वे नदियाँ जो एक ही राज्य में उसकी सीमाओं के अन्तर्गत पूर्णतया अर्थात् उद्गम स्थल से मुहाने तक बहती हैं। ये राष्ट्रीय नदी कही जाती हैं। जैसे-ब्रिटेन की टेम्स नदी।
(2) वे नदियाँ जो दो भिन्न राज्यों को एक-दूसरे से अलग करती हैं तथा दोनों राज्यों की सीमाओं को सृजित करती हैं।
(3) वे नदियाँ जो कई राज्यों से होकर बहती हैं, ऐसी नदियों को अनेक राष्ट्रीय नदियाँ या बहुर्राष्ट्रीय नदियाँ कहते हैं। इन्हें गैर राष्ट्रीय नदियों के रूप में भी जाना जाता है।
(4) वे नदियाँ जो खुले समुद्र से नोगम्य (navigable) होती हैं तथा उसी समय अपने उद्गम स्थल तथा अपने मुहाने के बीच या तो कई राज्यों को पृथक् करती हैं या कई राज्यों से होकर बहती हैं। गैर-राष्ट्रीय नदियों की तरह ये नदियाँ विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित हैं। लेकिन इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ माना जाता है, क्योंकि शान्ति के समय में यह सभी राज्यों के नौका-चालन के लिए खुली रहती है।
अन्तर्राष्ट्रीय नदियों तथा बहुराष्ट्रीय या गैर-राष्ट्रीय नदियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधि में यह नियम है कि राज्य नदी की प्राकृतिक धारा को परिवर्तित नहीं कर सकता, जो अन्य तटवर्ती राज्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। ओपेनहाइम के अनुसार “अन्तर्राष्ट्रीय नदी के प्रवाह को परिवर्तित करना तटवर्ती राज्यों में से किसी की मनमाना शक्ति के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का यह नियम है कि कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता यदि यह परिवर्तन पड़ोसी राज्य के राज्यक्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति के लिए हानिकारक है।
(5) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Sea-bed Authority) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से अभिसमय के राज्य पक्षकार भाग 11 में क्षेत्र के लिए स्थापित व्यवस्था और करार के अनुसार क्षेत्र में क्रियाकलापों को विशेषकर क्षेत्र के संसाधनों को प्रशासित करने की दृष्टि से संगठित तथा नियन्त्रित करेंगे। प्राधिकरण के मुख्य अंग सभा, परिषद् तथा सविचालय हैं। सभी में प्राधिकरण के सभी सदस्य होंगे, जबकि परिषद् में प्राधिकरण के 36 सदस्य होंगे। इनका निर्वाचन सभा द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण के सचिवालय में महासचिव तथा ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे जैसा प्राधिकरण उचित समझे। इन्टरप्राइजेज भी प्राधिकरण का मुख्य अंग होगा, जो क्षेत्र में क्रियाकलापों को निष्पादित करेगा। प्राधिकरण का प्रत्येक मुख्य अंग तथा इन्टरप्राइजेज उन शक्तियों तथा कार्यों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होंगे जो अभिसमय के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उन्हें प्रदत्त किये जाते हैं। इन मुख्य अंगों के अतिरिक्त, समुद्र तक विवाद कक्ष को स्थापित करने के लिए भी प्रावधान है। सविचालय में महासचिव तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे। महासचिव की नियुक्ति परिषद् की सिफारिश पर सभी द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी। महासचिव प्राधिकरण का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।
अभिसमय प्रावधान करता है कि क्षेत्र के संसाधनों का अन्वेषण तथा दोहन प्राधिकरण के सहयोग से इन्टरप्राइजेज द्वारा या व्यक्तिगत या राज्य इकाइयों द्वारा किया जायेगा। समुद्र तल क्रिया-कलापों की सम्पूर्ण श्रेणी तथा प्रणालीबद्ध संक्रिया के अन्य पहलू प्राधिकरण की परिषद् की सिफारिश पर प्राधिकरण की सभा द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले नियमों, विनियमों, तथा प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं। अभिसमय का संलग्न सामान्य शब्दों में योग्यता मानक को निर्दिष्ट करता है, जिसकी समुद्र तल संविदा को धारण करने वाले आवेदकों से माँग की जायेगी। उन्हें अभिसमय के राज्य पक्षकार या ऐसे राज्य द्वारा प्रयोजित इकाई होनी चाहिए जिन्हें प्राधिकरण की परिषद् द्वारा अग्रिम में परिभाषित किये जाने वाले वित्तीय तथा तकनीकी मापदण्डों को पूरा करना होता है तथा समुद्र तल क्रिया-कलापों पर प्राधिकरण के नियन्त्रण को स्वीकार करने के लिए सहमत होना पड़ता है। मूल पाठ में वर्णित प्रौद्योगिकी अन्तरण अपेक्षाओं का अनुसरण करना होता है।