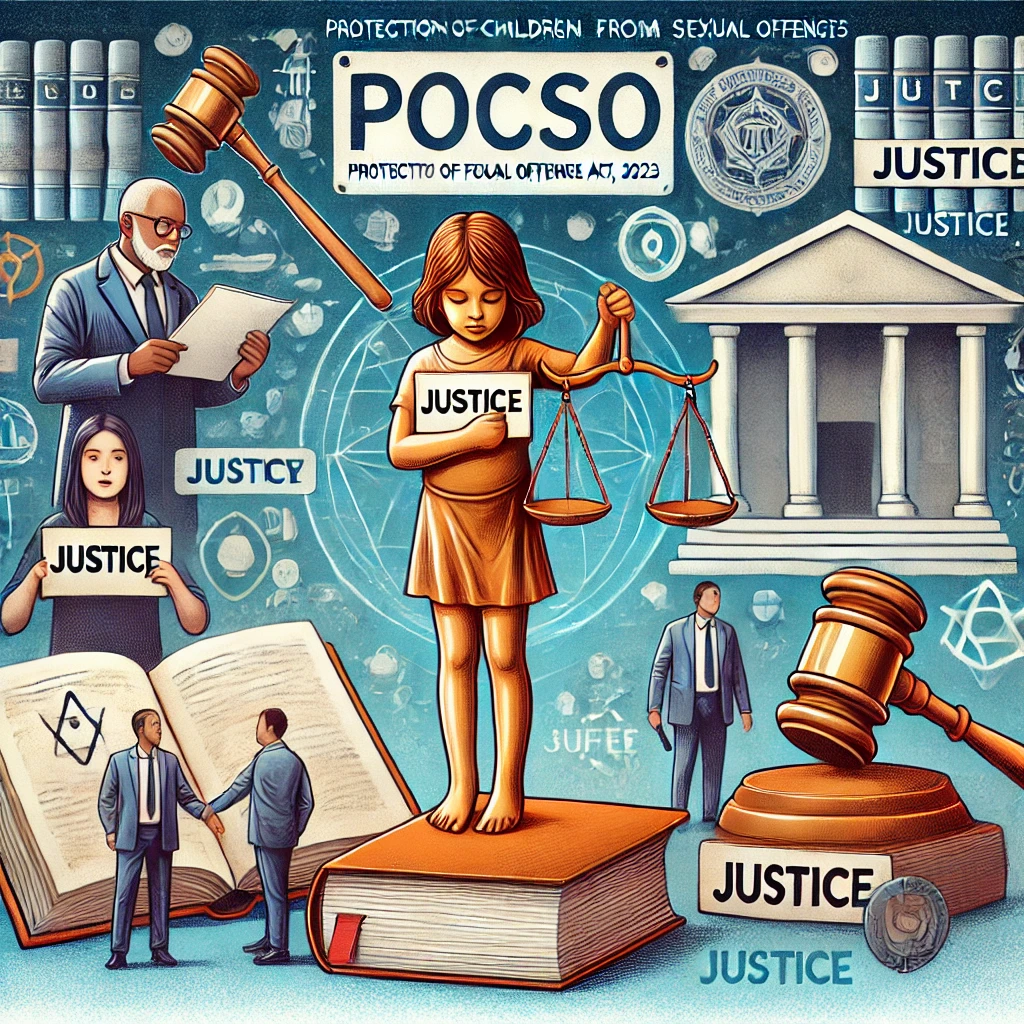शीर्षक: POCSO मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना: न्याय में शीघ्रता की दिशा में एक निर्णायक पहल
प्रस्तावना:
भारत में बच्चों के प्रति यौन अपराधों की बढ़ती घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय रही हैं। इन मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में होने वाली देरी, उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। इसी संदर्भ में, सरकार ने “POCSO अधिनियम, 2012” के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों (Fast Track Special Courts – FTSCs) की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया। यह पहल न केवल न्याय की त्वरित प्राप्ति सुनिश्चित करती है, बल्कि पीड़ितों में भरोसा और सामाजिक सुरक्षा की भावना भी पैदा करती है।
POCSO अधिनियम का संक्षिप्त परिचय:
“बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012” (POCSO Act) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अश्लील प्रदर्शन आदि से उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम बच्चों की विशेष संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए एक सुरक्षित और अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी?
हाल के वर्षों में POCSO के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में हजारों मामले लंबित हैं, जिनमें निर्णय आने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में पीड़ितों को न सिर्फ लंबे समय तक मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर से विश्वास भी कम होता जाता है।
इस पृष्ठभूमि में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना एक आवश्यक कदम बन गया, जिससे इन संवेदनशील मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और कार्य प्रणाली:
भारत सरकार ने 2019 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था – देश भर में 1023 विशेष अदालतों की स्थापना, जिनमें से अधिकांश को POCSO मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित किया गया।
इन अदालतों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:
- विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति: POCSO अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रशिक्षित न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
- मित्र अधिकारी (Support Person) की भूमिका: प्रत्येक पीड़ित को एक ‘मित्र अधिकारी’ प्रदान किया जाता है जो उन्हें अदालत की प्रक्रिया समझाने और भावनात्मक सहयोग देने में मदद करता है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा: बच्चों की सुविधा के लिए साक्ष्य के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी विकल्प अपनाए गए हैं।
- बंद कमरे में सुनवाई (In-camera trial): बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की उपलब्धियां:
इन अदालतों के माध्यम से अब कई मामलों में 6 महीने या उससे कम समय में ही निर्णय सुनाया गया है, जबकि पहले यही निर्णय वर्षों ले लेता था। उदाहरण के लिए, कुछ राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, जहां POCSO के मामलों में सजा की दर भी बढ़ी है।
विधिक और प्रशासनिक चुनौतियां:
हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने न्याय में गति लाई है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
- अपर्याप्त संख्या में न्यायाधीश: कई बार नियुक्तियाँ समय पर नहीं हो पातीं।
- साक्ष्य संग्रहण में देरी: पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी से मामलों की गति धीमी हो जाती है।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी: कई अदालतों में तकनीकी और भौतिक संसाधनों की कमी होती है।
- मानव संसाधन की कमी: प्रशिक्षित परामर्शदाता, मित्र अधिकारी और अभियोजन पक्ष की कमी एक बड़ी चुनौती है।
सुधार की संभावनाएं:
- फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना और प्रक्रिया को स्वचालित करना।
- पुलिस और अभियोजन पक्ष को यौन अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता एवं दक्षता का विशेष प्रशिक्षण देना।
- मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विधायी संशोधनों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाना।
न्यायिक सक्रियता और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार POCSO मामलों में न्याय में देरी को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्यों को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने, संसाधनों को बढ़ाने और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
निष्कर्ष:
POCSO मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारतीय न्याय प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुधार है। इससे जहां पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय मिल रहा है, वहीं समाज में एक मजबूत संदेश भी जा रहा है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन सरकार और न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के साथ यह पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है।
न्याय में देरी, न्याय से वंचना के समान होती है। इस पृष्ठभूमि में फास्ट ट्रैक अदालतें, भारत में बाल यौन अपराधों के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध का प्रतीक बन रही हैं।