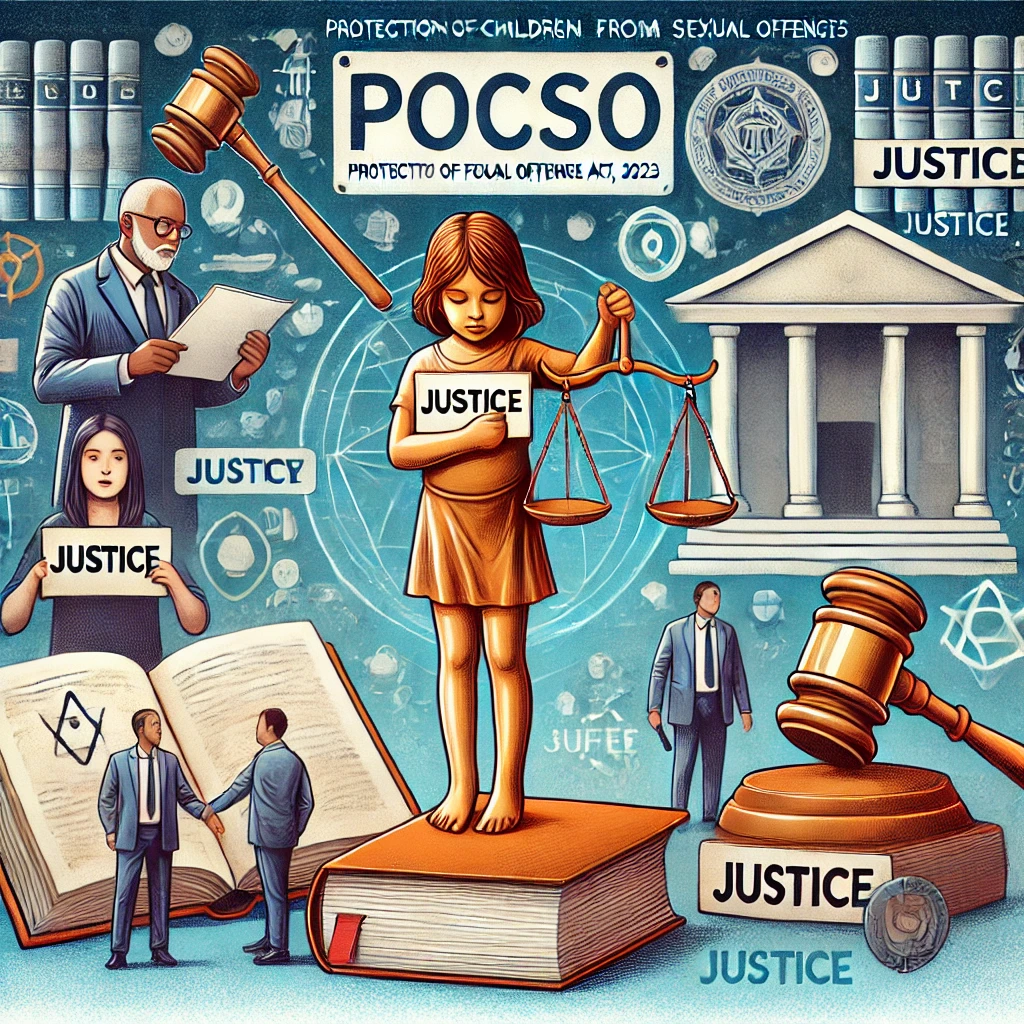POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रभावशीलता: बाल यौन शोषण के विरुद्ध त्वरित न्याय की पहल
परिचय:
भारत में बाल यौन शोषण की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं। बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट लागू किया गया। यह अधिनियम एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसमें बच्चों के प्रति यौन अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। यह लेख POCSO अधिनियम की संरचना, उद्देश्यों, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका की गहन विवेचना करता है।
POCSO अधिनियम का उद्देश्य एवं विशेषताएं:
POCSO अधिनियम 2012 बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता जैसे अपराधों से संरक्षण हेतु बनाया गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- लैंगिक तटस्थता – यह अधिनियम लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से संरक्षण देता है।
- परिभाषा की स्पष्टता – यौन हमला, अप्राकृतिक कृत्य, अश्लील प्रदर्शन आदि की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं।
- बच्चे की पहचान की गोपनीयता – मीडिया द्वारा पीड़ित की पहचान प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है।
- बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया – पूछताछ, मेडिकल जांच, और अदालत में बयान के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की अवधारणा:
POCSO मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में बाल यौन उत्पीड़न मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) स्थापित करने की योजना बनाई। इसके तहत देशभर में 1000 से अधिक विशेष अदालतें प्रस्तावित की गईं।
मुख्य उद्देश्य:
- मामलों का शीघ्र निपटारा करना
- पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना
- लंबित मामलों की संख्या कम करना
- पीड़िता के दोबारा ट्रॉमा से गुजरने की आशंका को न्यूनतम करना
POCSO मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की चुनौतियाँ:
हालाँकि POCSO अधिनियम प्रभावी है, फिर भी कई चुनौतियाँ सामने आती हैं:
- मामलों की अत्यधिक संख्या: प्रत्येक वर्ष हजारों मामले दर्ज होते हैं, जिससे न्याय प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
- प्रशिक्षण की कमी: पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को बाल अनुकूल तरीके से व्यवहार हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- समाज में कलंक: यौन शोषण की घटनाओं को लेकर सामाजिक बदनामी के डर से कई बार पीड़ित शिकायत ही दर्ज नहीं कराते।
- गवाही से मुकर जाना: लंबी न्याय प्रक्रिया और दबाव के कारण कई गवाह एवं पीड़ित अपने बयान से मुकर जाते हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की सफलता और प्रभाव:
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुछ हद तक न्याय प्रक्रिया में गति लाई है। कई राज्यों में मामलों का निपटारा 2 से 6 महीनों के भीतर हो रहा है। वर्ष 2023 तक लगभग 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील थीं, जिनमें से अधिकांश ने POCSO व बलात्कार जैसे मामलों को प्राथमिकता दी।
कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:
- मामलों की शीघ्र सुनवाई: POCSO के तहत दर्ज मामलों का औसतन निपटारा समय घटा है।
- सजा की दर में वृद्धि: पीड़िता की समय रहते गवाही और ठोस साक्ष्यों के कारण सजा दर में वृद्धि देखी गई।
- पीड़ित का मनोबल बढ़ा: त्वरित न्याय मिलने से पीड़ित एवं उनके परिवार को मानसिक संतोष मिलता है।
सुधार के सुझाव:
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता: पीड़ित बच्चों को परामर्श (काउंसलिंग) की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और चिकित्सा कर्मचारियों को POCSO के तहत उचित व्यवहार हेतु प्रशिक्षित किया जाए।
- डिजिटल सुनवाई: मामलों की सुनवाई में तकनीकी साधनों (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि) का उपयोग बढ़ाया जाए।
- जागरूकता अभियान: स्कूलों, गांवों, और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और अभिभावकों को यौन शोषण के विरुद्ध जागरूक किया जाए।
निष्कर्ष:
POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भारत में बाल यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, अभी भी न्याय प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील, त्वरित एवं बाल अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का सही उपयोग तभी संभव है जब पीड़ितों को पर्याप्त सहायता, संरक्षण और विश्वास प्रदान किया जाए। बच्चों की सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।