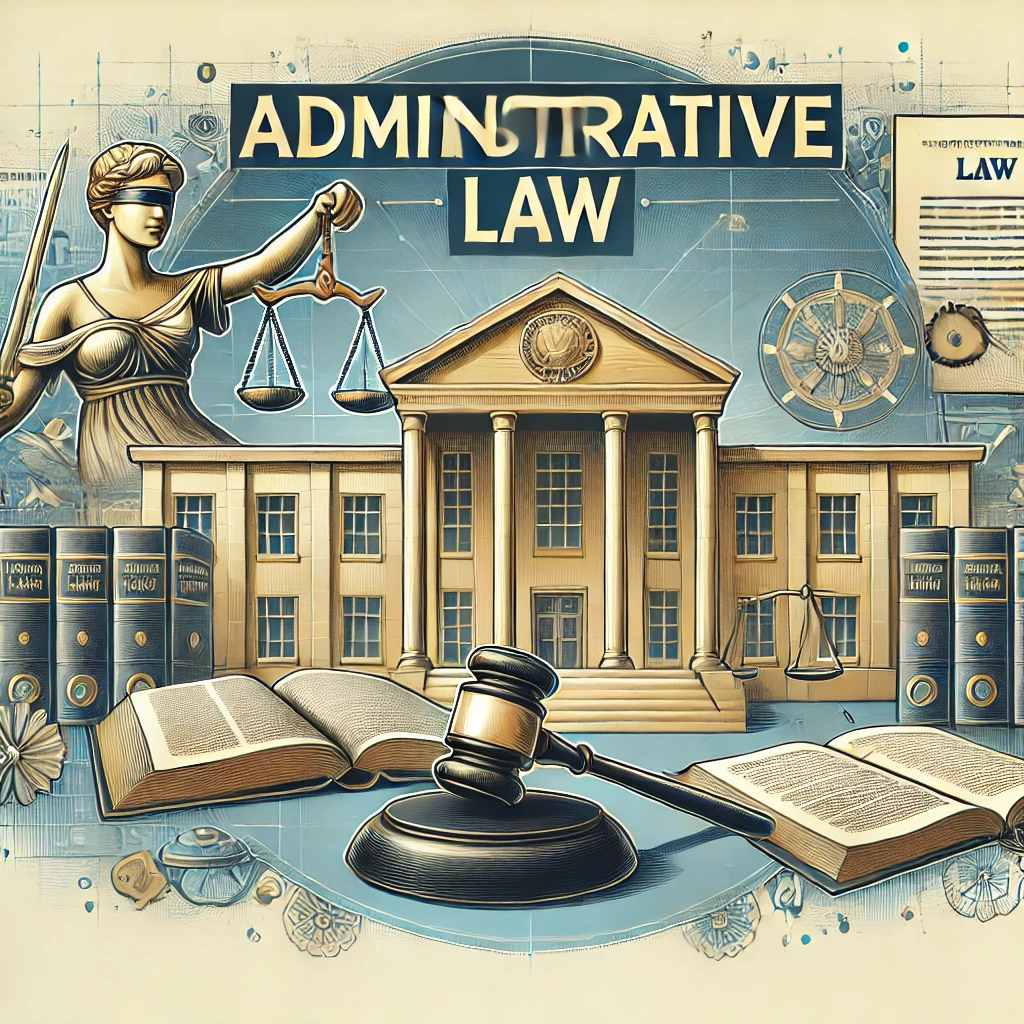Ombudsman और भारत में लोकपाल : एक विश्लेषण
प्रस्तावना
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वह जनता के प्रति कितनी जवाबदेह (Accountable) और पारदर्शी (Transparent) है। जब प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, तो भ्रष्टाचार, पक्षपात, कदाचार और मनमानी की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि एक स्वतंत्र संस्था हो, जो जनता की शिकायतों को सुने और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करे। इसी आवश्यकता की पूर्ति Ombudsman और भारत में लोकपाल जैसी संस्थाओं से होती है।
Ombudsman का अर्थ और उत्पत्ति (Meaning and Origin of Ombudsman)
“Ombudsman” शब्द स्वीडन (Sweden) की भाषा से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है – प्रतिनिधि (Representative) या Agent of the People।
- Ombudsman की उत्पत्ति 1809 में स्वीडन में हुई, जब वहाँ के संविधान में पहली बार Justitieombudsman नामक संस्था स्थापित की गई।
- इसका उद्देश्य था – नागरिकों की शिकायतों की जाँच करना और यह देखना कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन विधि और न्याय के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं।
धीरे-धीरे यह संस्था डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देशों में फैल गई। इसे भ्रष्टाचार विरोधी और प्रशासनिक न्याय का प्रभावी साधन माना गया।
Ombudsman की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Ombudsman)
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक/वैधानिक संस्था होती है।
- इसे सामान्यतः संसद या विधानसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसका कार्य है – प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी और नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई।
- यह सामान्यतः एक एकल प्राधिकारी होता है, जिसे लोकपाल (Lokpal) या लोकायुक्त (Lokayukta) कहा जाता है।
- यह सीधे जनता की शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है और संबंधित प्राधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
भारत में लोकपाल की अवधारणा (Concept of Lokpal in India)
भारत में Ombudsman की अवधारणा को “लोकपाल” (Lokpal) और “लोकायुक्त” (Lokayukta) के रूप में अपनाया गया।
- “लोकपाल” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में किया गया, जब एल.एम. सिंहवी (L.M. Singhvi) ने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया।
- इसके बाद 1966 में संतोष हेगड़े समिति और अन्य संसदीय समितियों ने इसके गठन की अनुशंसा की।
- कई बार संसद में लोकपाल विधेयक लाया गया, परंतु राजनीतिक कारणों से यह लंबे समय तक पारित नहीं हो सका।
अंततः 2013 में “लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013” (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) पारित हुआ।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)
मुख्य प्रावधान (Key Provisions)
- लोकपाल का गठन
- केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना।
- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य और 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे।
- नियुक्ति प्रक्रिया
- लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित न्यायाधीश) और एक विशिष्ट विद्वान की समिति द्वारा की जाएगी।
- अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)
- लोकपाल प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच कर सकता है।
- हालाँकि, प्रधानमंत्री के कुछ कार्य जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, परमाणु नीति आदि लोकपाल के दायरे से बाहर रहेंगे।
- जाँच और अभियोजन (Investigation and Prosecution)
- लोकपाल शिकायत मिलने के 60 दिनों में प्राथमिक जाँच कर सकता है।
- इसे सीबीआई और सीवीसी जैसी एजेंसियों से जाँच कराने का अधिकार है।
- दोष सिद्ध होने पर अभियोजन चलाया जा सकता है।
- राज्यों में लोकायुक्त
- अधिनियम के तहत राज्यों को अपने-अपने लोकायुक्त का गठन करना आवश्यक है।
भारत में लोकपाल का विकास (Evolution of Lokpal in India)
लोकपाल का गठन 2013 में हुआ, लेकिन वास्तव में यह संस्था 2019 में पहली बार कार्यशील बनी।
- मार्च 2019 में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (Justice Pinaki Chandra Ghose) को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया।
- वर्तमान में लोकपाल संस्था भ्रष्टाचार विरोधी शिकायतों की जाँच कर रही है, परंतु इसकी प्रभावशीलता को लेकर प्रश्न भी उठाए जाते हैं।
लोकपाल और लोकायुक्त के कार्य (Functions of Lokpal and Lokayukta)
- भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच।
- जाँच रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित प्राधिकरण को कार्रवाई हेतु भेजना।
- प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाना।
- जनसाधारण को त्वरित न्याय दिलाना।
- प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना।
लोकपाल और लोकायुक्त की विशेषताएँ (Salient Features of Lokpal in India)
- यह स्वतंत्र संस्था है, जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है।
- इसकी नियुक्ति बहुदलीय समिति द्वारा की जाती है।
- इसके सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि वाले और प्रशासनिक अनुभव वाले होते हैं।
- यह नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने का एक संवैधानिक साधन प्रदान करता है।
महत्व और आवश्यकता (Importance and Need)
- भ्रष्टाचार विरोधी हथियार – भारत जैसे देश में जहाँ प्रशासन में भ्रष्टाचार व्यापक है, वहाँ लोकपाल जैसी संस्था अनिवार्य है।
- नागरिकों की शिकायत निवारण – आम नागरिक को सीधी शिकायत दर्ज करने का अवसर मिलता है।
- निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच – लोकपाल स्वतंत्र होकर निष्पक्षता से जाँच कर सकता है।
- लोकतांत्रिक जवाबदेही – यह संस्था कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- जन विश्वास में वृद्धि – जब नागरिक देखते हैं कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है, तो शासन के प्रति विश्वास बढ़ता है।
आलोचनाएँ और सीमाएँ (Criticism and Limitations)
- प्रधानमंत्री पर सीमित अधिकार – प्रधानमंत्री के कुछ कार्य लोकपाल की पहुँच से बाहर हैं।
- स्वतंत्रता पर प्रश्न – लोकपाल की जाँच एजेंसियाँ (जैसे CBI) सरकार के अधीन होती हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- धीमी प्रक्रिया – शिकायतों की जाँच और कार्रवाई में समय लगता है।
- राज्यों में असमानता – कई राज्यों में लोकायुक्त प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे।
- दंड का अभाव – लोकपाल केवल अनुशंसा दे सकता है, अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में रहता है।
न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial Approach)
भारतीय न्यायपालिका ने हमेशा भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की आवश्यकता पर बल दिया है।
- Vineet Narain v. Union of India (1997) – सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सीवीसी को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता बताई।
- न्यायालयों ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता लोकतंत्र का मूल है, और लोकपाल जैसी संस्थाएँ इसे सुनिश्चित करने का साधन हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत में लोकपाल का विचार Ombudsman प्रणाली से प्रेरित होकर आया। लंबे संघर्ष और बहसों के बाद 2013 में यह अधिनियम पारित हुआ। यह भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है क्योंकि इसके अधिकार सीमित हैं और यह जाँच एजेंसियों पर निर्भर है। यदि इसे और अधिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और दंडात्मक शक्तियाँ दी जाएँ, तो यह संस्था भारत में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मजबूत नींव बन सकती है।
अतः सही कहा गया है –
“लोकपाल केवल एक संस्था नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता की आशाओं और विश्वास का प्रतीक है।”