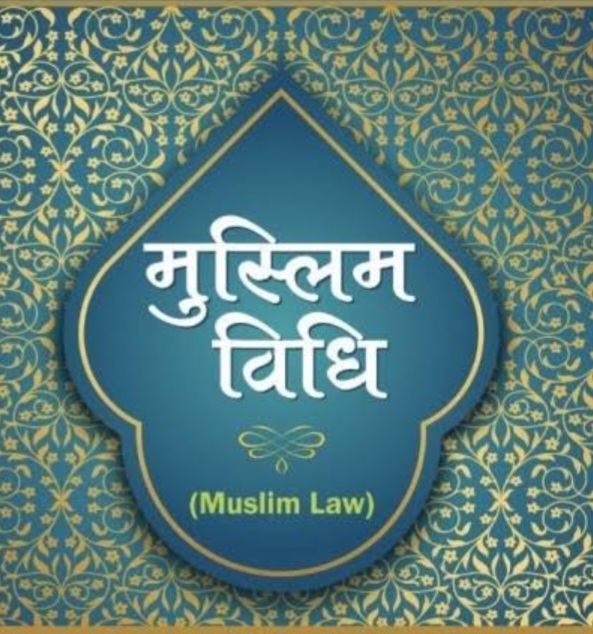-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
प्रश्न 1. (क) इस्लाम के आगमन के पूर्व अरब की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। Describe briefly the special conditions of Arabia before the advent of Islam.
(ख) मुस्लिम विधि के स्वरूप को बतलाइये। मुस्लिम कौन होता है। निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। Discuss the nature of Muslim law. Who is Muslim? Explain with the help of decided cases.
उत्तर (क) – किसी देश की विधि प्रणाली (Legal System) – उस देश की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह सही भी है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे सामाजिक ढाँचे का निर्माण करने तथा उसको एक विशेष स्परूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक धारणायें, विश्वास, मत, रहन-सहन के ढंग, आदतें, खान-पान, रीति-रिवाज और यहाँ तक कि भाषा का निर्धारण भी भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा होता है।
अरब की जलवायु सदा से मानव जीवन के प्रतिकूल रही है। जल की कमी तथा गर्मी की अधिकता के कारण, बालू के रेगिस्तानों के कारण और उपज की न्यूनता के कारण वहाँ के निवासियों का जीवन अति दुष्कर है। आधुनिक नगरों में बसने वाले उन कठिन परिस्थितियों में रहने वालों की जीवनचर्चा की कठिनाइयों के विषय में ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। पशुओं के लिए जल एवं चारागाहों की खोज में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे घूमते रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले परिश्रमी तथा विश्वसनीय होते हैं। यदि उनकी भूमि उनके प्रति उदार नहीं है तो वे स्वयं उदारता को एक महान् गुण मानते हैं। साहस एवं वीरता उनके जन्मजात गुण हैं।
प्राचीन अरब के निवासी सामूहिक रूप से रहते थे। अपने पशुओं और स्त्रियों की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझते थे। अधिकांश विद्वानों का मत है कि प्राचीन अरब में स्त्रियों की स्थिति पशुओं से अधिक ऊँची नहीं थी। उनके कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें चल सम्पत्ति के समान माना जाता था। विवाह के पूर्व पिता और विवाहोपरान्त पति स्त्री को जिस प्रकार चाहते उस प्रकार रखते थे। बहु-विवाह एक प्रचलित प्रथा थी। मोहम्मद साहब के लगभग 100 वर्ष पूर्व अरब देश में मध्यम वर्ग की सभ्यता थी। अरब में स्त्रियों के साथ अच्छा एवं मानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे तथा थोड़ी स्वतंत्रता भी थी। शनैः-शनै: यह सभ्यता लोप होती गयी और अरब के निवासियों ने अपना धर्म विस्तृत कर दिया। उनकी नैतिक भावना का लोप हो गया और उनमें एक प्रकार मूर्तिपूजा की प्रथा प्रचलित) हो गयी।
विधि को धर्म से जोड़ दिया गया। विधिशास्त्र के अन्तर्गत ‘विधि’ को अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है अर्थात् विधि की कोई सारभूत परिभाषा नहीं है इसीलिए विधि को परिभाषा के लिए अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ।
जैसे-विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, समाजवादी यथार्थवादी विचारधारा आदि विश्लेषणात्मक विचारधारा में ‘विधि’ को सम्प्रभु का समादेश माना गया, ऐतिहासिक विचारधारा में विधि को रूढ़ि से जोड़ा गया और कहा गया कि विधि समाज में पहले से विद्यमान रहती है इसे बनाया नहीं जाता है, प्राकृतिक विचारधारा के विधिशास्त्रियों के विधि को ईश्वरी देन माना, जबकि समाजवादी विचारधारा में विधि को सामाजिक अभियांत्रिकी के रूप में तथा यथार्थवादी विचारधारा में विधि को न्यायपालिका की देन माना गया अर्थात् विधि एक ऐसा व्यादेश है जिसमें समाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखा जाता है जिन्हें समाज के प्रत्येक नागरिक को मानना बाध्यकारी होता है अर्थात् विधि के अन्तर्गत ही एक शाखा मुस्लिम विधि की भी है मुस्लिम विधि का धर्म से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् मुस्लिम विधि धर्म पर आधारित विधि है मुस्लिम विधि का धर्म से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् मुस्लिम विधि धर्म पर आधारित विधि है मुस्लिम विधि के अन्तर्गत जो विधि, उपविधि, नियम, विनियम बनाये गये हैं वह कुरान पर आधारित है तथा इसके साथ ही साथ पैगम्बर मुहम्मद साहब द्वारा जैसा आचरण एवं व्यवहार किया गया वे सभी विधि का रूप धारण कर लिए। वर्तमान में लगभग सभी वैयक्तिक विधियों में सुधार देने को बल मिल रहा है किन्तु मुस्लिम विधि में नाममात्र का ही सुधार सम्भव हो सका है क्योंकि मुस्लिम विधि धर्म से इतना अधिक जुड़ी है कि उसमें कोई घड़ा परिवर्तन कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा है।
उत्तर (ख ) – मुस्लिम विधि की प्रकृति (Nature of Muslim law)— किसी देश की विधि प्रणाली (Legal System) उस देश की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह सही भी है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे सामाजिक ढाँचे का निर्माण करने तथा उसको एक विशेष स्परूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक धारणायें, विश्वास, मत, रहन-सहन के ढंग, आदतें, खान-पान, रीति-रिवाज और यहाँ तक कि भाषा का निर्धारण भी भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा होता है।
अरब की जलवायु सदा से मानव जीवन के प्रतिकूल रही है। जल की कमी तथा गर्मी की अधिकता के कारण, बालू के रेगिस्तानों के कारण और उपज की न्यूनता के कारण वहाँ के निवासियों का जीवन अति दुष्कर है। आधुनिक नगरों में बसने वाले उन कठिन परिस्थितियों में रहने वालों की जीवनचर्या की कठिनाइयों के विषय में ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। पशुओं के लिए जल एवं चारागाहों की खोज में वे एक-स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे घूमते रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले परिश्रमी तथा विश्वसनीय होते. हैं। यदि उनकी भूमि उनके प्रति उदार नहीं है तो वे स्वयं उदारता को एक महान् गुण मानते हैं। साहस एवं वीरता उनके जन्मजात गुण हैं।
प्राचीन अरब के निवासी सामूहिक रूप से रहते थे। अपने पशुओं और स्त्रियों की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझते थे। अधिकांश विद्वानों का मत है कि प्राचीन अरब में स्त्रियों को स्थिति पशुओं से अधिक ऊँची नहीं थी। उनके कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें चल सम्पत्ति के समान माना जाता था। विवाह के पूर्व पिता और विवाहोपरान्त पति स्त्री को जिस प्रकार चाहते उस प्रकार रखते थे। बहु-विवाह एक प्रचलित प्रथा थी। मोहम्मद साहब के लगभग 100 वर्ष पूर्व अरब देश में मध्यम वर्ग की सभ्यता थी अरब में स्त्रियों के साथ अच्छा एवं मानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे तथा थोड़ी स्वतंत्रता भी थी। शनैः-शनै: यह सभ्यता लोप होती गयो और अरब के निवासियों ने अपना धर्म विस्तृत कर दिया। उनकी नैतिक भावना का लोप हो गया और उनमें एक प्रकार मूर्तिपूजा की प्रथा प्रचलित हो गयी। विधि को धर्म से जोड़ दिया गया।
विधिशास्त्र के अन्तर्गत ‘विधि’ को अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है अर्थात् विधि की कोई सारभूत परिभाषा नहीं है इसीलिए विधि की परिभाषा के लिए अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ।
जैसे- विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, समाजवादी यथार्थवादी विचारधारा आदि विश्लेषणात्मक विचारधारा में ‘विधि’ को सम्प्रभु का समादेश माना गया, ऐतिहासिक विचारधारा में विधि को रूढ़ि से जोड़ा गया और कहा गया कि विधि समाज में पहले से विद्यमान रहती है इसे बनाया नहीं जाता है, प्राकृतिक विचारधारा के विधिशास्त्रियों के विधिः को ईश्वरी देन माना, जबकि समाजवादी विचारधारा में विधि को सामाजिक अभियांत्रिकी के रूप में तथा यथार्थवादो विचारधारा में विधि को न्यायपालिका की देन माना गया अर्थात् विधि एक ऐसा व्यादेश है जिसमें समाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखा जाता है जिन्हें समाज के प्रत्येक नागरिक को मानना बाध्यकारी होता है अर्थात् विधि के अन्तर्गत हो एक शाखा मुस्लिम विधि को भी हैं मुस्लिम विधि का धर्म से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् मुस्लिम विधि धर्म पर आधारित विधि है मुस्लिम विधि का धर्म से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् मुस्लिम विधि धर्म पर आधारित विधि है मुस्लिम विधि के अन्तर्गत जो विधि, उपविधि, नियम, विनियम बनाये गये हैं वह कुरान पर आधारित है तथा इसके साथ ही साथ पैगम्बर मुहम्मद साहब द्वारा जैसा आचरण एवं व्यवहार किया गया वे सभी विधि का रूप धारण कर लिए। वर्तमान में लगभग सभी वैयक्तिक विधियों में सुधार देने को बल मिल रहा है किन्तु मुस्लिम विधि में नाममात्र का हो सुधार सम्भव हो सका है क्योंकि मुस्लिम विधि धर्म से इतना अधिक जुड़ी है कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा है।
मुसलमान कौन हैं— मुस्लिम विधि में मुसलमान वह व्यक्ति होता है जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है तथा उसका अनुपालन करता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य इस्लाम के पाँच स्तम्भों पर केन्द्रित है, ये स्तम्भ है-
1. पूर्ण आस्था (Full Faith ) – “मुसलमान” शब्द का अर्थ होता है “मुसलमान- ईमान” मुसल्लम ईमान से तात्पर्य है पूर्ण आस्था यहाँ पूर्ण आस्था से तात्पर्य कुरान के कलमा में पूर्ण आस्था “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद-उर-रसूल अल्लाह” अर्थात् खुदा एक है और एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं और मोहम्मद साहब खुदा के दूत थे।
2. नमाज (प्रार्थना) – यह मुस्लिम धर्म का दूसरा स्तम्भ है। प्रत्येक दिन पाँच बार (प्रातः दोपहर, दोपहर के पश्चात्, सूर्यास्त और रात्रि) में मक्का की ओर अपना मुख कर विहित नमाज को पढ़े। शुक्रवार को दोपहार का नमाज सभी पुरूषों के लिए आवश्यक है कि उसे सामूहिक तौर पर पढ़े।
3. दान देना (Alms-giving) – अपनी आय के कुछ भाग का गरीबों, सन्तों को दान करना और पुण्यार्थ संस्थायें चलाना।
4. रोजा रखना (व्रत) — इस उद्देश्य के लिए रमजान का मास सबसे पवित्र माना गया है और प्रत्येक मुस्लिम को प्रातः काल से सूर्यास्त तक सभी भोजन, पानी आदि से विरत रहना चाहिए।
5. हज (तीर्थयात्रा ) – इस्लाम धर्म का यह अन्तिम स्तम्भ है। जीवन में एक बार प्रत्येक मुस्लिम को जो व्यय करने में समर्थ हो, वर्ष के एक विहित समय में मक्का का पवित्र दर्शन अवश्य करे।
अमीर अली ने मोहम्मडन लॉ नामक पुस्तक में कहा कि वह व्यक्ति मुस्लिम है जो दो बातों- तौहीद और रसूल में विश्वास करता है, अर्थात् प्रथमतः यह कि खुदा एक है और एक के सिवाय दूसरा नहीं, दूसरी बात यह कि मोहम्मद साहब खुदा के दूत या रसूल थे। यह न्यूनतम आस्था अपरिहार्य (आवश्यक) है। यदि इससे कम पर आस्था है तो वह व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, और यदि इससे अधिक है तो वह अनावश्यक जब तक किसी व्यक्ति का विश्वास तौहीद और रसूल व खुदा एक है, तब तक न्यायालय को इससे मतलब नहीं कि वह कट्टरपंथी है या उदारवादी या वह अन्य किन-किन वस्तुओं या सिद्धान्तों में आस्था रखता है।
अहमदिया लोग आधुनिकतावादी और गैर-कट्टरपंथी मुस्लिम हैं। ये लोग मजहब के नाम पर किये जाने वाले युद्ध की निन्दा करते हैं और उनका कहना यह है कि मोहम्मद साहब ख़ुदा के पैगम्बर अवश्य थे किन्तु वह अन्तिम पैगम्बर नहीं थे, उनके पश्चात् भी कोई पैगम्बर अवतरित हो सकते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद में आस्था रखना धर्म में आस्था है और बिना इस आस्था के मजहब पूर्ण नहीं होता है।
नारन्तकथ बनाम पारक्कल, ए० आई० आर० 1923 मद्रास 171 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अहमदिया लोग मुस्लिम हैं क्योंकि वे लोग “तौहीद” और ” रसूल” दोनों को मानते हैं। इस वाद में पारक्कल नामक एक मोपला महिला ने एक पुरुष से विवाह किया। इस विवाह के कुछ दिनों के बाद ही वह पुरुष अहमदिया सम्प्रदाय में शामिल हो गया। मोपला लोग रूढ़िवादी सम्प्रदाय के लोग होते हैं इस कारण जब पति अहमदिया हो गया तो उसके इस कार्य को धर्म-परिवर्तन समझा गया। जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार जब कोई मुस्लिम पुरुष अपना धर्म त्याग दे तो उसका विवाह विच्छेद स्वतः हो जाता है इस समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए मोपला महिला ने समझा कि उसका विवाह विच्छेद हो गया इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। मुसलमानों के लिए यह सार्वजनिक महत्व का प्रश्न बन गया। एक मत था कि द्विविवाह नहीं था जब कि अहमदिया जो अपने-आपकों सदा से मुसलमान मानते आये हैं, का मत था कि महिला द्वारा जो दूसरा विवाह किया गया था वह द्वि-विवाह था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि कोई मुसलमान अहमदिया हो जाये तो उसका मतलब यह नहीं होता कि उसने अपना धर्म-परिवर्तन कर लिया है और वह अब मुसलमान नहीं रहा है और इसलिए महिला द्वारा दूसरी शादी करना कानून की दृष्टि में अपराध था।
जीवन खाँ बनाम हबीब (1933) 14 लाहौर 518 के वाद में यह तर्क उठाया गया कि शिया समुदाय के लोग मुसलमानों के प्रथम तीन खलीफा को नहीं मानते हैं इसलिए वे लोग मुसलमान नहीं हैं इस पर लाहौर उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि शिया लोगों का विश्वास सुन्नियों के विश्वास से भिन्न है, परन्तु वे लोग भी इस्लाम के आवश्यक तत्वों
तौहीद और रसूल अर्थात् “खुदा एक है और एक के सिवा कोई नहीं, तथा मोहम्मद साहब ख़ुदा के रसूल थे” पर पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं अतः शिया सम्प्रदाय के लोग भी मुस्लिम या मुसलमान माने जायेंगे।
प्रश्न 2. मुस्लिम विधि मुसलमानों पर किन मामलों में लागू होती है? मुस्लिम धर्म स्वीकार करने तथा परित्याग करने पर किसी व्यक्ति के विधिक हैसियत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट करें। In what matters the Muslim Law is applicable to Muslim? What is the effect of conversion to Muslim religions and apostasy from Muslim religions on the legal status of Person ?
उत्तर – भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात् भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। – भारत में विधायिका द्वारा निर्मित विधि सामान्यतया सभी लोगों पर लागू होती है। अपवाद के रूप में वैयक्तिक विधियाँ एवं कुछ विशिष्ट विधियाँ आती हैं जो सीमित लोगों एवं सीमित स्थानों पर लागू होती हैं। मुसलमानों के कुछ वैयक्तिक अधिकारों पर मुस्लिम विधि लागू होती है वे निम्नलिखित है –
1. विवाह (Marriage)
2. विवाह विच्छेद (Divorce)
3. उत्तराधिकार (Succession)
4. वसीयत (Will)
5. दान (Gift)
6. वक्फ (Waqf)
7. दहेज (मेहर) (Dower)
अभिभावकता (Guardianship) तथा पैतृकता (Paternity) भरण पोषण, संरक्षकता, पूर्व-क्रयाधिकार, दाय प्राप्ति आदि के सम्बन्ध में मुसलमानों पर लागू होती है। जिन मामलों में अब मुस्लिम विधि लागू है उनमें भी यह विधि काफी हद तक संशोधित और परिवर्तित हो गई है।
मुस्लिम विधि न केवल उन लोगों पर लागू होती है जो जन्म से मुसलमान हैं वस्तु उन लोगों पर भी लागू होती है जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी धर्म का परित्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसके ऊपर पुराने धर्म की विधि लागू नहीं होती है। इस्लाम धर्म में परिवर्तित होते ही उसके ऊपर मुस्लिम विधि लागू होने लगती है। मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) प्रयोग अधिनियम, 1937 के प्रावधान के अनुसार मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकार के मामले में किसी प्रथा या रूढ़ि का सहारा नहीं ले सकता है।
किन्तु मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) प्रयोग अधिनियम, 1937 के लागू होने के पूर्व मुसलमानों की अतियाँ खोजा, कुची मेमन, हलाई मेमन, सुन्नी बोहरा प्रभागत उत्तराधिकार विधि से प्रशासित होती थी जो कि हिन्दू विधि की तरह थी।
मुस्लिम विधि पर सर्वप्रथम प्रमाणित पुस्तक मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरियत) प्रयोग अधिनियम, 1937 बना जो 7 अक्टूबर, 1937 से सारे भारत में लागू हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू हो, और शुद्ध मुस्लिम विधि के विरूद्ध जो प्रचलित रिवाज और प्रथाये हों वे सब समाप्त हो जायें। निर्वसीयत उत्तराधिकार से सम्बन्धित मुस्लिम विधि के विरोध में प्रचलित प्रथायें ही मुख्य दोष थे जिसका निराकरण करना अधिनियम का मुख्य ध्येय था। इस अधिनियम में कुल 6 धारायें दी गई है।
इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में होगा यह बात इस अधिनियम के धारा-1 में कही गई है। धारा-2 यह कहती है कि किसी प्रतिकूल रिवाज या प्रथा के होते हुए भी सभी मामलों में (कृषि भूमि से सम्बन्धित विषयों को छोड़कर) चाहे निर्वसीयती उत्तराधिकार का हो, या स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति का हो जिसमें संविदा या दान या वैयक्तिक विधि के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त या दायप्राप्त की गई निजी सम्पत्ति भी शामिल है, चाहे विवाह हो, या विवाह विच्छेद जिसमें तलाक, इला, जिहार लिआन, खुला और मुबारत भी शामिल है, चाहे भरण-पोषण, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास एवं न्यास सम्पत्ति तथा वक्फ चाहे ऐसा वक्फ खैरात, पुण्यार्थ संस्थाओं, और पुण्यार्थ एवं धमार्थ धर्म दायों से भिन्न से सम्बन्धित सभी वादों में जहाँ सभी पक्षकार मुस्लिम हो, ऐसे मामलों का निपटारा करने की विधि मुस्लिम वैयक्तिक विधि जिसे शरीयत भी कहते हैं, होगी।
मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) प्रयोग अधिनियम-1937 की धारा-2 के प्रावधान अनिवार्य रूप से सभी मुसलमानों पर लागू होंगे, किन्तु धारा-3 के प्रावधान तभी लागू माने जायेंगे जब वे इस बात की घोषणा प्राप्त करेंगे कि वे इस धारा के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं।
मोहम्मद असलम खाँ बनाम खलीलुल रहमान ए० आई० आर० 1947 पी० सी० 97 के बाद में प्रिवी कौंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) प्रयोग अधिनियम, 1937 की धारा-2 का उद्देश्य यह है कि मुस्लिम विधि के विरोध में कुछ मुस्लिम जातियों में प्रचलित जो रिवाज या प्रथायें है उन्हें निरस्त कर दिया जाय।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा भारत का अपना एक संविधान है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं उन्हीं मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है ” धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार” जिसके बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उपबंध किया गया है। अनुच्छेद-25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान | हक की गारन्टी प्रदान करता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म (मजहब) को ग्रहण कर सकता है। जब कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे ‘इस्लाम धर्म में परिवर्तन” (Conversion) कहा जाता है, और जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना मजहब छोड़ देता है तो उसे “इस्लाम धर्म के परित्याग” (Apostasy) की संज्ञा दी जाती है। मुस्लिम विधि के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जन्म से मुस्लिम हो यदि वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी धर्म परिवर्तन द्वारा है तो भी यह पर्याप्त है। यह बात अब्राहम बनाम अब्राहम, (1863) 9 मूर इण्डियन अपील्स 195 के बाद में कही गयी है।
मुस्लिम धर्म में परिवर्तन का वैवाहिक अधिकारों पर प्रभाव- मुस्लिम विधि के अनुसार पति-पत्नी में से जब कोई एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है तो दो परिस्थितियों पर विचार किया जाता है कि –
(i) क्या यह ऐसे देश में किया गया है जो मुस्लिम विधि के अधीन है, या
(ii) ऐसे देश में किया गया है जहाँ कि मुस्लिम विधि देश की विधि नहीं है।
पहले मामले में जब पति-पत्नी में से एक इस्लाम धर्म ग्रहण करे तो उसे चाहिए कि दूसरे पक्ष से वह इस्लाम धर्म ग्रहण करने को कहे और दूसरा पक्ष यदि इस्लाम धर्म ग्रहण न करे या इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इन्कार कर दे तो विवाह विच्छेद न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किन्तु दूसरे मामले में, पति-पत्नी में से किसी एक के द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने के तीन मास व्यतीत हो जाने पर विवाह का स्वतः विच्छेद हो जाता है। यद्यपि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कि मुस्लिम विधि देश की विधि नहीं है, फिर भी ऐसी विधि भारत में लागू नहीं है। जहाँ पति-पत्नी में से कोई एक व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले तो धर्म परिवर्तित व्यक्ति विवाह विच्छेद के लिए न तो न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और न ही वह इस प्रकार की घोषणा ही प्राप्त कर सकता है कि उसका विवाह सम्बन्ध उस पक्षकार से समाप्त हो गया जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया है।
सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० 1995 एस० सी० 1531 के मामले में हिन्दू पति जो पहले से ही शादीशुदा था उसने अपनी पत्नी से बिना विवाह विच्छेद किये ही मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया तथा एक अन्य मुस्लिम महिला से – ‘निकाह’ कर लिया। यहाँ पर यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसा विवाह मान्य होगा? इस पर उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि ऐसे व्यक्ति ने केवल अपने लैंगिक सम्बन्धों को जायज करने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था जबकि उसका इरादा दुराशयपूर्ण था। इस कारण पहले विवाह के जारी रहते हुए मुस्लिम महिला से किया गया विवाह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 सपठित धारा 17 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत द्विविवाह (Bigamy) की परिभाषा में आता है अतः ऐसा विवाह शून्य विवाह माना जायेगा।
इसी प्रकार एक मामलें लिली थामस बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए० आई० आर० 2000 एस० सी० 1650 में श्रीमती सुष्मिता घोष एवं श्री जी० सी० घोष का विवाह हिन्दू धर्म के अनुसार 10 मई, 1984 को नई दिल्ली में हुआ था और तब से दोनों पक्ष खुशी पूर्वक विवाहित जीवन बिता रहे थे। अप्रैल, 1992 में पति ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे अपने हित में पारस्परिक सहमति से तलाक ले लेना चाहिए क्योंकि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसका नाम मुहम्मद करीम गाजी हो गया है तथा वह तलाकशुदा श्रीमती विनीता गुप्ता जो दो बच्चों की माँ है के साथ जुलाई, 1992 में विवाह करेगा। मुहम्मद करीम गाजी ने अपनी पत्नी श्रीमती सुष्मिता घोष को काजी द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का प्रमाण-पत्र भी दिखाया। काफी प्रयास करने पर भी पति-पत्नी का विवाद नहीं हल हो सका। अन्ततः पत्नी श्रीमती सुष्मिता घोष ने पीड़ित हिन्दू महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने वाली संस्था “कल्याणी” से सम्पर्क किया तथा संस्था के अध्यक्ष की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विपक्षी / पति द्वारा किये जाने वाले विवाह को रोकने का अनुरोध स्वीकार किया गया इसके बावजूद भी उसने श्रीमती विनीता के साथ विवाह कर लिया और दूसरी पत्नी से 27 मई, 1993 को अस्पताल में पुत्र उत्पन्न हुआ जिसमें बच्चे के जन्म प्रमाण- पत्र के साथ श्री जी० सी० घोष तथा माता का नाम “विनीता घोष” धर्म ‘हिन्दू’ लिखा गया था। उक्त प्रमाण पत्र पत्नी सुष्मिता घोष द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर दाखिल किया गया। उपरोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विपक्षी पति ने केवल दूसरा विवाह करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया है न कि उसे मुस्लिम धर्म में आस्था है और इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को दुराशय होने के कारण अवैध माना गया क्योंकि पति ने मात्र अपने लाभ या शारीरिक सुख के लिए “इस्लाम” स्वीकार कर लिया था। अतः उसका पति द्विविवाह का दोषी माना जायेगा।
दाय प्राप्ति के अधिकार पर प्रभाव (Effect of conversion on inheritance)—दाय प्राप्ति के मामलों में, किसी प्रतिकूल रूढ़ि के अभाव में, इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले की सम्पत्ति का उत्तराधिकार मुस्लिम विधि द्वारा शासित होता है, और मुस्लिम विधि के अनुसार कोई गैर-मुस्लिम मुसलमान की सम्पदा का हकदार नहीं होता है।
चेदम्बरम बनाम मा नेयन ए० आई० आर० 1928 रंगून 179 के मामले में एक हिन्दू ने जिसके पत्नी और बच्चे थे, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और एक मुस्लिम महिला से विवाह किया और उससे भी बच्चे हुए। जब वह व्यक्ति मर गया तो पत्नियों और बच्चों में सम्पत्ति- प्राप्ति के विषय में विवाद उठा। यह निर्णीत हुआ कि मृतक की सम्पदा उसके मुस्लिम पत्नी और मुस्लिम पत्नी से उत्पन्न बच्चों को मिलेगी, हिन्दू पत्नी और उनके बच्चे सम्पदा में हिस्सा न प्राप्त करेंगे, क्योंकि मुसलमान की सम्पत्ति का कोई हिन्दू उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है।
प्रश्न 3. मुस्लिम विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा उसकी विभिन्न विचार पद्धतियों (Schools) में इन स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए।
या
मुस्लिम विधि के स्त्रोत क्या हैं? निम्नलिखित में से किन्हीं दो की मुस्लिम विधि के स्रोतों के रूप में व्याख्या कीजिए:
(1) कुरान (2) सुन्ना, (3) विधायन ।
Explain the main sources of Muslim Law and their relative importance in variuos schools.
OR
What are the sources of Muslim Law? Explain any two of the following as sources of Muslim Law:
(1) Quram, (2) Sunna, (3) legislation.
उत्तर- मुस्लिम विधि एक धार्मिक विधि है। मुस्लिम विधि इस्लाम के सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आज भी मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं जिन्हें सभ्य समाज स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। मुस्लिम विधि सिर्फ चौदह सौ वर्ष पुरानी है। मोहम्मद साहब के माध्यम से ईश्वर के आदेश तथा मुहम्मद साहब के आचरण के आधार पर मुस्लिम विधि के सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है।
मुस्लिम विधि का जन्म कैसे हुआ अर्थात् कौन-कौन से कारक (Factors) मुस्लिम विधि को मूर्त स्वरूप देने के लिए उत्तरदायी हैं, इस आधार पर मुस्लिम विधि के स्रोतों को प्रमुखतः दो भागों में बाँटा जा सकता है –
(1) प्राचीन स्रोत,
(2) आधुनिक स्रोत
(1) प्राचीन या परम्परागत स्रोत
मुस्लिम विधि के चार प्रमुख प्राचीन या परम्परागत स्रोत है (1) कुरान (Quran). (2) सुन्नत तथा हदीस (Sunnat and Hadis), (3) इज्मा (ljma) (4) कियास (Qiyas).
(2) आधुनिक स्रोत- (1) प्रथाएँ तथा रूढ़ियाँ (Customs and usages), (2) न्यायिक विनिश्चय (Judicial decisions), (3) विधायन (Legislation), (4) न्याय, साम्या एवं सद्विवेक (Justice, Equity and good
(1) कुरान (Quran)
कुरान मुस्लिम विधि का सबसे प्रमुख एवम् सर्वमान्य स्रोत है। मुस्लिम वर्ग कुरान से हटकर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कुरान का जन्म अरबी शब्द करा से हुआ है। करा शब्द का अर्थ है – पढ़ना या उच्चारित करना। कुरान में वे सभी बातें संग्रहीत हैं जो मुहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के लिए उच्चारित की थीं।
मुहम्मद साहब को जबराइल (Gabriel) के माध्यम से खुदा (ईश्वर) का संदेश प्राप्त होता था। यह संदेश कभी-कभी मुहम्मद साहब को निद्रा में तथा कभी-कभी अर्द्ध-विक्षिप्त अवस्था में प्राप्त होता था। मुहम्मद साहब को जो ईश्वरीय संदेश निद्रा या अर्द्ध-विक्षिप्त अवस्था में प्राप्त होता था उसे उन्होंने लोगों को बताया। कुरान मुहम्मद साहब द्वारा बताए गए इन संदेशों का लिपिबद्ध रूप है। यह स्मरणीय है कि कुरान मुहम्मद साहब के जीवन काल में लिपिबद्ध नहीं हुआ किन्तु स्मरण के आधार पर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात् ही उनके द्वारा बतायी गई बातों को लिपिबद्ध किया जा सका। मोहम्मद साहब को प्राप्त ईश्वरीय संदेश जो उन्होंने लोगों को बताया ताम्रपत्रों, पत्थरों, वृक्षों की छालों या अन्य वस्तुओं पर अंकित थे। मोहम्मद साहब को मृत्यु के पश्चात् खलीफा अबू बकर ने इन संदेशों को एकत्र करने का कार्य मोहम्मद साहब के शिष्य जैद को सौपा। अबू बकर ने यह संग्रह अपनी पुत्री तथा मोहम्मद साहब की विधवा हफजा को सौंपा। मुसम्मात हफजा के पास से प्राप्त कुरान की प्रति को आधार मानकर जैद साहब ने एक प्रति तैयार की। यही सही एवम् प्रामाणिक प्रति मानी गई। उससे कई अन्य प्रतियाँ बनवाकर इस्लामी देशों में प्रेषित की गई। यही प्रतियाँ मूल तथा प्रामाणिक प्रतियाँ मानी गयी तथा अन्य प्रतियाँ जला दी गई। खलीफा उस्मान द्वारा जैद साहब के माध्यम से तैयार कराई गई प्रति आज भी अपरिवर्तित रूप में उपलब्ध है।
कुरान में मोहम्मद साहब को प्राप्त ईश्वरीय संदेश संग्रहीत हैं जो उन्होंने अपने लोगों को उच्चारित किया। कुरान एक सौ चौदह (114) सुरा या अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों को क्रमांकित करने का आधार उनका आकार है। कुरान में मजहब (Religion), नीतिशास्त्र (Ethics) तथा राजनीतिशास्त्र (Politics) की बातें संग्रहीत हैं। वैसे तो कुरान में विधि विषयक पाँच सौ आठ (508) आयतें (पाठ) हैं परन्तु इनमें से सिर्फ अठहत्तर आयतें ही ऐसी हैं जिन्हें न्यायाधीश तथा विधिविशेषज्ञ प्रयोग करते हैं। इन आयतों में विवाह, तलाक, मेहर तथा उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रावधान संग्रहीत हैं। कुरान सही रूप में विधिक संग्रह नहीं है क्योंकि इसमें विधि सम्बन्धी प्रावधान एक स्थान पर न होकर कई स्थानों पर बिखरे पढ़े हैं। फिर भी जिन विषयों का उल्लेख कुरान में है वे बाते इस मामले पर अन्तिम हैं। जैसे बहुपत्नीत्व के बारे में कुरान कहता है
“जो स्त्रियाँ तुमसे राजी हों उनसे तुम विवाह कर लो, दो, तीन या चार तलाक तथा तलाक के पश्चात् तलाकशुदा स्त्री से उसी पुरूष के साथ विवाह जिसने तलाक दिया है। कुरान की आज्ञा इस प्रकार है-
“पति ने पत्नी को तिबारा (तीसरी बार) तलाक दे दी, तत्पश्चात् जब तक वह (तलाकशुदा) स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह न करे तब तक वह स्त्री उस पति के लिए जायज नहीं है। हाँ यदि दूसरा पति विवाह (सम्भोग) करके उस स्त्री को तलाक दे दे तो उन दोनों (तलाकशुदा स्त्री तथा पुरूष) में कुछ पाप नहीं है कि वे एक दूसरे से विवाह- बन्धन में पुनः बंध जायें।”
विवाह के बारे में कुरान का आदेश है –
तुम्हारी माताएँ, पुत्रियाँ, बहनें बुआयें मौसियों, भतीजियाँ, भान्जिय तुम्हारी धात्रियों, जिन्होंने तुम्हे दूध पिलाया है, तुम्हारी धात्रेय बहनें, तुम्हारी सासें तुम्हारे लिए हराम हैं। तुम्हारी पत्नी से उत्पन्न पुत्र की पत्नी तथा दो बहनों का साथ-साथ पत्नी रखना तुम्हारे लिए हराम है।
सारांश में कहें तो कुरान में जितना विधि-विषय मिलता है उतना किसी भी धार्मिक ग्रन्थ में नहीं मिलता फिर भी कुरान आधुनिक विधि संहिता के रूप में नहीं है। परन्तु जिन बातों का उल्लेख कुरान में हैं वे अन्तिम हैं। कुरान में वर्णित विधि के निर्वाचन के बार में प्रिवी कौसिल द्वारा निर्णीत आगा मोहम्मद बनाम कुलसुम बीबी, (1897) का वाद उल्लेखनीय है जिसमें अभिनिर्धारित हुआ था कि न्यायालय कुरान के किसी नियम को निर्वाचित नहीं करेगे जहाँ वह हेदाया या इमामिया द्वारा निर्वाचित हो चुका हो।
(2) सुन्नत तथा हदीस (Sunnat and Hadis)
कुरान मुस्लिम विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुरान के पश्चात् सुन्नत तथा हदीस मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सुन्नत एकवचन है जिसका बहुवचन सुन्ना है। सुन्ना का तात्पर्य मोहम्मद साहब के आचरण से है। मुहम्मद साहब का आचरण इस प्रकार अनुकरणीय माना गया कि उनकी आचरण संहिता मुसलमानों के लिए कानून बन गयी। हदीस शब्द का अर्थ है प्रवचन। हदीस का बहुवचन है अहादी। अहादी से तात्पर्य मोहम्मद साहब द्वारा किये गये प्रवचनों से है। मुस्लिम विधि में सुन्नत तथा हदीस एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। परन्तु सुन्नत से तात्पर्य मोहम्मद साहब के कार्य-कलापों से है। मोहम्मद साहब का जीवन अनुकरणीय था तथा अपने प्रवचन तथा उपदेश के दौरान जो बाते उन्होंनें कही वह भी नियम के रूप में ग्रहणीय थे। अतः सुन्नत तथा हदीस मोहम्मद साहब के आचरण (जीवन- शैली) तथा उनके प्रवचनों-उपदेशों से संकलित नियम बन गये। उमय्या काल में मुहम्मद साहब के आचरण तथा उपदेश एवं प्रवचनों को लिपिबद्ध किया गया। मुहम्मद साहब के आचरण तथा प्रवचन मोहम्मद साहब के जीवन काल में संकलित नहीं किए गए, इन्हें विभिन्न व्यक्तियों ने अपने नजरिये से लिपिबद्ध किया। ये व्यक्ति मोहम्मद साहब के सहयोगी (साथी) थे। मुसलमान मोहम्मद साहब के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आचरण के कारण इन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूप से लिपिबद्ध किये गये सुन्ना तथा अहादी को बिना किसी जाँच अथवा प्रश्न के मानते थे।
चूँकि सुन्ना तथा अहादी मोहम्मद साहब के जीवन के पश्चात् उनके विभिन्न साथियों द्वारा लिपिबद्ध किये गये अतः यह स्वाभाविक था कि हदीसों के अनेक संग्रहों का अस्तित्व हो गया। सुन्नी सम्प्रदाय के हदीसों में सबसे महत्वपूर्ण हदीस बोखारी का है। इन्हें बोखरा के निवासी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल ने लिपिबद्ध किया था। उन्होने दैवी प्रेरणा से छः लाख से अधिक हदीसों का संग्रह किया, परन्तु इनमें से सत्य एवम् प्रामाणिक हदीस सिर्फ तीन हज़ार (3000) हदीस अबू अब्दुल्ला ने बताये हैं।
शिया सम्प्रदाय भिन्न हदीस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे सुन्नी सम्प्रदाय के हदीस पर विश्वास नहीं करते। बोखारी ने सुन्नी सम्प्रदाय के हदीसों को लिपिबद्ध करते समय उन हदीसों को पृथक कर दिया जिन्हें शिया सम्प्रदाय के पक्ष में उन्होंने माना। शिया सम्प्रदाय के हदीसों का संग्रह अबू जफर मोहम्मद तथा शेख अली ने किया। शिया सम्प्रदाय के लोग उन हदीसों पर विश्वास नहीं करते जिन्हें ऐसे व्यक्ति ने लिपिबद्ध किया हो जिसका सम्बन्ध मोहम्मद साहब के परिवार से न रहा हो।
हदीस का महत्व मोहम्मद साहब द्वारा अपनी मृत्यु शैय्या से दिये गये उपदेश से स्पष्ट है। मोहम्मद साहब ने मरने से पूर्व कहा था-“मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जय – तक तुम उन पर चलते रहोगे वे तुम्हें गलतियों से बचाती रहेंगी। वे दो वस्तुएं हैं:
खुदा की किताब (कुरान) तथा मेरी सुन्नत (आचरण) ।
मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में हदीस तथा कुरान को समान स्थान प्राप्त है। हदीस कुरान में लिखी बातों को स्पष्ट करते हैं परन्तु हदीस कुरान में लिखी बातों को निरस्त या पलट नहीं सकते। इस प्रकार हदीस तथा कुरान सिद्धान्त यदि परस्पर विरोधी है तो कुरान के सिद्धान्त को वरीयता दी जायेगी।
सुन्नत को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
(1) सुन्नत – उल – फेल – अर्थात् मोहम्मद साहब के स्वयं के आचरण।
(2) सुन्नत-उल-कौल- जिन्हें मोहम्मद साहब ने दूसरे को करने को कहा ।
(3) सुन्नत-उल- तकरीर – ऐसे आचरण जो मोहम्मद साहब के जीवन काल में व्यवहार में लाये गए तथा जिनका मोहम्मद साहब के द्वारा विरोध नहीं किया गया।
सुन्ना की भाँति अहादी को भी तीन भागों में बाँटा गया है-
(1) अहदिस-ए-मुतवासिर – सर्वसाधारण में प्रचलित तथा सर्वसामान्य द्वारा प्रमाणित (सार्वभौमिक परम्पराएँ)
(2) अहृदिस-ए-मशहूर – ऐसे हदीस जो सर्वसाधारण को ज्ञात है परन्तु उन्हें सर्वधारण के रूप में प्रसिद्धि नहीं मिली (लोकप्रिय परम्पराएँ)
(3) अहदिस-ए-अहद- ऐसे हदीस जो इक्का-दुक्का व्यक्तियों को ज्ञात हैं।
(3 ) इज्मा (Ijma)
कुरान तथा सुन्ना हदीस के पश्चात् मुस्लिम विधि का प्रामाणिक स्रोत इज्मा है। जिस विषय पर कुरान तथा हदीस एवम् सुन्नत में उल्लेख नहीं मिलता वहाँ इज्मा महत्वपूर्ण हो जाता है। इज्मा का शाब्दिक अर्थ है-एकमत होना। मुस्लिम विधिशास्त्र में इज्मा का आशय मोहम्मद साहब के सहयोगियों, उनके शिष्यों तथा शिष्यों की सहमति है। इज्मा का अर्थ है किसी समय मोहम्मद साहब के अनुयायियों में से विधिशास्त्रियों का किसी विधि के प्रश्न पर एकमत होना। इज्मा का प्रामाणिक आधार है-हदीस की एक उक्ति-उस हदीस में लिखा है- मेरे लोग जो मेरे अनुयायी हैं किसी ऐसी बात पर एकमत नहीं हो सकते जो गलत है।
यद्यपि इज्मा के आधार पर निर्मित नियम भिन्न-भिन्न मुस्लिम सम्प्रदायों में भिन्न हैं, परन्तु यह सुस्थापित है कि एक बार यदि एक इज्मा स्थापित या सर्वमान्य हो गया तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। सुन्नी सम्प्रदाय की हनाफी विचारधारा को मानने वालों के लिए इज्मा एक मूल तथा प्रमुख स्रोत है।
सर्वप्रथम खलीफा अबू बकर ने विधि के बिन्दु पर कई समस्याओं को इज्मा के आधार पर हल किया। उनके पश्चात् खलीफा उमर ने इज्मा को अपनाया। इज्मा के आधार पर दिये गए निर्णय फतवा कहे गये तथा इन फतवाओं को इस्लामी देशों में प्रेषित किया गया। इज्मा को तीन भागों में विभक्त किया गया है-
(1) मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा,
(2) विधिशास्त्रियों का इज्मा,
(3) सर्वसाधारण (जनता) का इज्मा
(1) मोहम्मद साहब के साथियों का इज्मा– मुस्लिमों के दोनों प्रमुख सम्प्रदाय-सुन्नी तथा शिया इस इज्मा को सबसे अधिक प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि चूँकि ये लोग मोहम्मद साहब के अधिक निकट रहते थे अतः उन्होंने मोहम्मद साहब की भाँति ही तर्क को अपनाया था। इसके लिए यह आवश्यक था कि इन इज्माओं को विश्वसनीय लोगों द्वारा समर्थन दिया गया हो।
(2) विधिशास्त्रियों का इज्मा– मोहम्मद साहब के सहयोगियों के इज्मा के पश्चात् विधिशास्त्रियों के इज्मा को प्रमुखता प्राप्त है। इस वर्ग में किसी एक कालखण्ड में विद्यमान विधिशास्त्रियों के किसी विषय पर मतैक्य को रखा गया है। अधिकांश हनफी सम्प्रदाय के नियम उसी वर्ग के इज्मा द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं।
इज्मा को स्वीकार करने के पीछे यह तर्क है कि किसी बात पर एक व्यक्ति तो त्रुटि कर सकता है परन्तु कई व्यक्ति किसी ऐसे बात पर मतैक्य (सहमति) नहीं जताते जो सत्य न हो तथा यदि कई विधिवेत्ता किसी एक बात पर सहमत हो जायें तो अत्यधिक सम्भावना रहती है। कि वह त्रुटि से मुक्त है या उसके त्रुटि की सम्भावना न्यूनतम रहती है। इज्मा ने मुस्लिम विधि की निर्माण-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा मुस्लिम विधि का विकास स्थगित नहीं हुआ।
(3) जनता (People’s) का इज्मा – मुस्लिम जनता के द्वारा सर्वमान्य सिद्धान्त अर्थात् ऐसे नियम जिन पर साधारण जनता सहमत है वह जनता का इज्मा कहलाया। यह मुस्लिम जनता की धर्म-विषयक सहमति है। यद्यपि जनता के इज्मा को विशेष महत्व प्राप्त नहीं है परन्तु प्रार्थना तथा धार्मिक विषय पर जनता द्वारा अपनाये गए नियम इस वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
(4) कियास (Qiyas) — कियास का शाब्दिक अर्थ है तार्किक निष्कर्ष (Logical decisions) कियास, कुरान सुन्नत तथा हदीस एवं इज्मा के पश्चात् मुस्लिम विधि का चौथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किवास के अन्तर्गत मुस्लिम विधिशास्त्री किसी सुस्थापित इस्लामिक नियम को ऐसे मामलों पर तर्क के आधार पर लागू करते हैं जिस पर पूर्व में ऐसा नियम लागू नहीं था। इस प्रकार कियास किसी नवीन विधि या नियम की रचना नहीं करता बल्कि पुराने सुस्थापित सिद्धान्त जो कुरान, हदीस या इज्मा के आधार पर सुस्थापित हो गए हैं उन्हें विधिशास्त्री नई परिस्थितियों में लागू करते हैं।
कियास को मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अबू हनीफा को दिया जाता है। अबू हनीफा ने क़ियास को नया रूप देकर इसका नामकरण इज्तिहाद के रूप में किया जिसकी तुलना अंग्रेजी विधि के सिद्धान्त साम्या (Equity) के साथ की जा सकती है। कियास के अन्तर्गत विधि के सुस्थापित नियमों को न्याय की मांग के अनुसार नवीन मामलों पर लागू किया जाता है। जिस मामले के बारे में कुरान, सुन्नत तथा हदीस एवं इज्मा के अन्तर्गत कुछ नहीं कहा गया है उस मामले पर तर्क के आधार पर विधिशास्त्रियों ने कुरान सुन्नत तथा हदीस एवं इज्मा के सिद्धान्तों को लागू किया है। इस तरह कियास ने मुस्लिम विधि के नवीन नियमों का विकास किया। इस प्रकार मुस्लिम विधि, विधायिका कार्य का संग्रहजनित न होकर विधिवेत्ताओं के विचारों (कियास) द्वारा जनित एक विज्ञान है।
मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विक्रय के लिए यह आवश्यक है कि जिस वस्तु का विक्रय होना है उसका अस्तित्व (Existence) हो परन्तु कियास उस संविदा को शून्य नहीं मानता जिसके अन्तर्गत किसी वस्तु का निर्माण कर उसका विक्रय करने का वचन दिया गया हो क्योंकि साम्या की यह माँग है कि इस प्रकार का वचन आम तौर पर प्रचलित होने के कारण मान्य किया जाय।
इसी प्रकार यदि कोई मुसलमान अपने पीछे सिर्फ पुत्रियाँ ही छोड़कर मरता है तो मुस्लिम विधि के अनुसार यदि एक पुत्री है तो उसे 1/2 भाग प्राप्त होगा, यदि दो से अधिक पुत्रियाँ हैं तो सभी पुत्रियाँ मिलकर 2/3 भाग प्राप्त करेंगी, परन्तु यदि सिर्फ दो पुत्रियाँ हैं तो प्रत्येक पुत्री कितना प्राप्त करेगी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अत: कियास या तर्क द्वारा विधिशास्त्रियों ने दो या दो से अधिक पुत्रियों का एक ही अर्थ लगाया तथा यह नियम प्रतिपादित किया कि यदि कोई मुसलमान दो या दो से अधिक पुत्रियाँ अपने पीछे छोड़कर मरता है तो सभी पुत्रियाँ मिलकर कुल सम्पत्ति का 2/3 भाग ही प्राप्त करेंगी।
सुन्नी शाखा की हनबली विचारधारा के लोग तथा शिया सम्प्रदाय के लोग कियास को अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि उनके अनुसार विधि की व्याख्या या विधि का विस्तार सिर्फ धार्मिक मुखिया या इमाम द्वारा ही किया जाना चाहिए।
यह उल्लेखनीय है कि कियास द्वारा किसी भी परिस्थिति में कुरान सुन्नत तथा हदीस एवं इज्मा द्वारा निर्धारित नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता कियास समय में परिवर्तन के साथ-साथ विधि के परिवर्तन का एक साधन है। इस प्रकार कियास विधि की स्थापना में तो समर्थ नहीं है परन्तु सुस्थापित विधि को तर्क के आधार पर न्याय की माँग के अनुसार विधि के नियमों को स्पष्ट कर नवीन परिस्थतियों पर पुरानी विधि को इस प्रकार लागू करने में सहायक है कि पुरानी विधि में मूलभूत परिवर्तन न हो।
(2) मुस्लिम विधि के आधुनिक स्त्रोत
(1) प्रथा या रिवाज (Customs) तथा रूड़ियाँ या रीतियाँ (Usages) हिन्दू विधि की तरह मुस्लिम विधि के विकास में भी प्रथा तथा रूढ़ियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनको तामुल उर्फ या रिवाज के नाम से भी जाना जाता है। प्रथा एवं रीतियाँ या रूढ़ियाँ ऐसे नियमों या आचरणों का संग्रह हैं जो किसी विशिष्ट कालखण्ड में किसी विशेष स्थान के विशिष्ट समुदाय द्वारा पालन की जाती हैं। प्रथा तथा रूढ़ियों को विधि का बल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इनका पालन अविस्मरणीय समय से निरन्तर किया जा रहा हो तथा यह अनैतिक या समाज के हितों के प्रतिकूल न हो। उदाहरण के रूप में हम पाते हैं कि पंजाब तथा गुजरात में कुछ वर्ग (खोजा समुदाय) के मध्य हिन्दू रीति-रिवाजों का पालन आज भी हो रहा है तथा इस सीमा तक इन वर्गों में मुस्लिम विधि परिवर्तित हो गई है। प्रिवी कौंसिल ने भी अब्दुल हुसैन बनाम सीनाडेरो, (1917) 45 इण्डियन अपील्स 10 नामक वाद में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मूल ग्रन्थ के लिखित कानून (Written law) की तुलना में रीति-रिवाजों को वरीयता मिलेगी। मुसलमानों में बहुविवाह, मेहर, तलाक, मौखिक वसीयत आदि का विकास रिवाज (प्रथाओं) तथा रीतियों के आधार पर ही हुआ है।
(2) न्यायिक विनिश्चयन (Judicial decisions)
पूर्व न्यायिक विनिश्चयन जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले में किये जाते हैं वे उसी प्रकार के तथ्यों पर निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। परन्तु चूँकि विधि का निर्माण न्यायालयों द्वारा नहीं होता है अतः पूर्व न्यायिक निर्णयों को सही रूप में विधि का स्रोत नहीं मानना चाहिए परन्तु किसी विशिष्ट मामले में निर्णय करते समय अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों से मार्ग- निर्देशित होते हैं। इस प्रकार सन् 1950 तक प्रिवी कौंसिल, तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम विधि के कई सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। वे उन्हीं तथ्यों पर भविष्य के मामले के लिए बाध्यकारी सिद्धान्त बन गये हैं तथा पूर्व न्यायनिर्णय विधि का एक स्रोत बन गया है।
(3) विधायन (Legislation)
विधायन, मुस्लिम विधि ही नहीं बल्कि सबल विधियों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विधायन द्वारा विधि का निर्माण तथा अन्त दोनों होता है। मुस्लिम विधि मुसलमानों के धार्मिक पुस्तक कुरान पर आधारित विधि है। यद्यपि मुस्लिम सम्प्रदाय अपनी वैयक्तिक विधि में ऐसे परिवर्तन, जो कुरान में प्रतिपादित नियमों से विसंगत हैं, से उद्वेलित हो उठता है परन्तु फिर भी विधायिका के प्रयत्नों द्वारा मुस्लिम विधि में ऐसे परिवर्तन सम्भव हुए हैं जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं थे।
विधायिका द्वारा मुस्लिम विधि में किए गए कुछ परिवर्तनों का उल्लेख निम्नलिखित है-
(1) कुरान में पूर्व विवाहिता से विवाह हराम घोषित है परन्तु दासियों से विवाह की अनुमति है, भले ही वे पूर्व विवाहित हों। परन्तु सन् 1843 में भारत में दास- प्रथा का उन्मूलन हो गया। अब दासियों की प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया है।
(2) मुस्लिम विधि में धर्म-परिवर्तन पर प्रतिबन्ध है तथा यदि कोई मुस्लिम अपना धर्म-परिवर्तन करता है तो उसे अपने परिवार में उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ता है। जाति-निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 (The Caste Disabilities Removal Act, 1850) ने मुस्लिम विधि के इस नियम को निरस्त कर अब यह प्रावधान किया है कि अब कोई मुस्लिम अपने धर्म- परिवर्तन के पश्चात् भी परिवार में प्राप्त उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
(3) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कोई मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद (Divorce) या तलाक की माँग नहीं कर सकती। परन्तु सन् 1939 में विधायिका द्वारा पारित मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के आधार पर अब कुछ आधारों पर एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अब मुस्लिम विवाहित पति-पत्नी में से एक धर्म-परिवर्तन करके भी पति-पत्नी के रूप में बने रह सकते हैं जबकि पूर्व में मुस्लिम पति या पत्नी में से किसी द्वारा धर्म-परिवर्तन उनके वैवाहिक सम्बन्ध को समाप्त कर देता था।
इसी प्रकार विधायिका द्वारा पारित मुस्लिम वक्फ विधिमान्य करण अधिनियम, 1913, शरीयत अधिनियम, 1937, वक्फ अधिनियम, 1954 तथा मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा विधायिका ने मुस्लिम विधि में व्यापक परिवर्तन किया है।
यद्यपि विधायिका द्वारा पारित अधिनियम मुस्लिमों पर लागू हैं परन्तु व्यवहार में मुस्लिम सम्प्रदाय अपने कुरानिक विधि से शासित होना अधिक पसंद करता है, सिवाय आपराधिक मुस्लिम विधि के भारत में अब सामान्य विधि लागू करने की चर्चा है जो सभी धर्मों के व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो।
न्याय, साम्या एवं सद्विवेक (Justice, equity and good conscience ) — प्रिवी कौंसिल ने हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी, (1916) के मामले में कहा कि “मुस्लिम विधि के ग्रन्थों में काजी के कर्तव्यों से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विधि सामान्यतया अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा साम्या एवं साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और मुकदमों के न्याय निर्णयन में उनका अनुसरण किया जाता है और इसे इस्तिहसान के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 4. (i) न्यायिक निर्णय के महत्व की मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप मेंbविस्तृत व्याख्या कीजिए । Discuss the significance of ‘Precedent’ as a source of Muslim Law in detail.
(ii) विधायन के महत्व की मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में विस्तृत व्याख्या कीजिए। Discuss the significance of ‘Legislation’ as a source of Muslim Law in detail.
उत्तर- (i) इंग्लैण्ड की भाँति भारत में भी न्यायिक निर्णयों को बड़ा महत्व प्रदान किया जाता है। पूर्व न्यायिक निर्णय से तात्पर्य यहाँ यह लगाया जाता है कि भूतकाल के निर्णयों का भविष्य में आने वाले निर्णयों के पथ-प्रदर्शन के रूप में उपयोग किया जाय। वास्तविकता तो यह है कि पूर्व न्यायिक निर्णय उस तरह का विधि का स्रोत नहीं है जैसा विधायन क्योंकि न्यायाधीश का कार्य विधि निर्माण न होकर उसका निर्वचन करना ही है। विधि के विकास में न्यायिक निर्णयों के निर्वाचन का बहुत महत्व है। किसी विशेष विवाद में किसी विधि को लागू करने और उसका अर्थान्वयन करने में न्यायाधीशगण व्यक्त या अव्यक्तरूपेण यह घोषित करते हैं कि अमुक परिस्थिति में कौन-सी विधि लागू की जायेगी और उसके क्या परिणाम होंगे। तत्पश्चात् होने वाले विवादों में यह निर्णय बाध्यकारी सत्ता के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रिवी कौंसिल द्वारा दिया गया निर्णय भारत के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होता था किन्तु अब स्वतन्त्र भारत में प्रिवी कौंसिल का स्थान उच्चतम न्यायालय ने ले लिया है। लगभग 100 वर्षों तक प्रिवी कौंसिल ने और सन् 1950 ई० से उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम विधि वादों पर सैकड़ों निर्णय दिये हैं। वे निर्णय अब मुल्लम विधि के स्रोत बन गये हैं। वे निर्णय उसी प्रकार की परिस्थितियों में भविष्य में आने वाले मुकदमों में मान्य विधि के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।
कुरान तथा हदीस में जो मुस्लिम विधि पर चीजें दी हुई हैं या जैसा कि इज्मा या कियास द्वारा प्रकटित है वह विधि कई विषयों पर शान्त थी और इस कारण प्रिवी कौंसिल तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को इस कमी को निर्णयार्थ आये विवादों के सिलसिले में पूरा करना पड़ता था। न्यायालय यह घोषित करता था कि उस विषय पर क्या विधि होगी या लागू होगी। ब्रिटिश काल में अंग्रेज न्यायाधीश को अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान न होने पर तथा गलत निर्णय से बचने के लिए उन्होंने पूर्व निर्णयों का सहारा लिया।
ख्वाजा हुसेन अली बनाम शहजादी हजारी बेगम (1969) 12 वीकली रिपोर्ट्स के मामले में न्यायाधीश मारक्वी ने यहाँ तक कहा कि- “इस न्यायालय के पास मुस्लिम विधि के अन्वेषण का साधन अति कम है और इतना सीमित है कि मुस्लिम विधि से सम्बन्धि किसी विषय पर अपने विचार न प्रकट करने में मुझे प्रसन्नता होती है।”
न्यायिक निर्णयों ने अनेक विषयों में शुद्ध सम्पत्ति जिसका विभाजन नहीं हो सकता, का दान मुशा का दान कहलाता है जो मुस्लिम विधि के अनुसार वैध और मान्य होता है। किन्तु जो सम्पत्ति विभाज्य है उस सम्पत्ति के अविभाजित सम्पत्ति का दान मान्य नहीं है विभाजन करके ही ऐसी सम्पत्ति का दान किया जाना चाहिए। न्यायिक निर्णय द्वारा ‘अविभाज्य सम्पत्ति’ में ऐसी सम्पत्ति भी शामिल कर ली गई है जिसका विभाजन तो हो सकता है किन्तु जिसके विभाजन होने से उस सम्पत्ति का मूल्य या महत्व के घटने की सम्भावना हो।
मोहम्मद मुमताज बनाम जुवेदा जान (1889) 16 इण्डियन अपील्स के मामले में यह मत प्रकट किया गया कि “मुस्लिम विधि में मुशा के दान को अमान्य मानना समाज की प्रगतिशील अवस्था के बिल्कुल ही प्रतिकूल है और इस कारण नियम को जितना भी सीमित किया जा सके उतना ही सीमित रखा जाये।
(2) आजीवन सम्पदा-अमजद खाँ बनाम अशरफ खाँ, आ० इ०रि० 1929 प्रिवी काँसिल 194 के मामले में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि सुन्नी शाखा की मुस्लिम विधि में आजीवन सम्पदा के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था उसे बदलकर या उस विधि में परिवर्तन करके यह धारण किया गया कि आजीवन हित का दान सुन्नी विधि के अंतर्गत भी मान्य है और ऐसा आजीवन हित बढ़कर पूर्ण स्वामित्व सम्पदा नहीं हो जाता है।
(3) विधवा द्वारा कब्जा बनाये रखने का अधिकार-जिस विधवा के मेहर की धनराशि बकाया है उसे मुस्लिम विधि में मेहर की माँग को लागू कराने के सम्बन्ध में विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। जब मुस्लिम विधवा ने मेहर के एवज में पति की सम्पत्ति पर कब्जा किया हो तो जब तक उसकी बकाया मेहर की राशि अदा न कर दी जाए, तब तक वह उत्तराधिकारियों के विरुद्ध सम्पत्ति का कब्जा धारण किये रहने की हकदार है। मेहर की एवज में पति की सम्पत्ति को अपने पास रोक रखने के विधवा के इस अधिकार को न्यायिक निर्णयों ने काफी बढ़ा दिया है।
हुसेन बनाम रहीम खाँ, आ० इ० रि० 1954 मैसूर 24 एवं अब्दुल वहाब बनाम मुश्ताक अहमद, ए० आई० आर० 1944 इला० 63 तथा मुसम्मात हलीमन बनाम मुनीर, ए० आई० आर० 1971 पटना 385 नामक वादों में यह कहा गया कि अब यह अधिकार विधवा तक ही सीमित न होकर दाययोग्य (Heritable) हो गया है। इस नई विधि द्वारा अवयस्क और असहाय बच्चों की स्थिति असुरक्षित ऋणदाताओं की तुलना में अच्छी तथा बेहतर हो गई है।
(4) वक्फ – विधि की दृष्टि में वक्फ की सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति होती हैं। मुस्लिम विधि में प्राइवेट वक्फ एवं पब्लिक वक्फ में कोई अंतर नहीं है। दोनों किस्म के वक्फ का सृजन सदैव के लिए होता है और वक्फ की सम्पत्ति असंक्राम्य होती है। किन्तु न्यायिक निर्णयों ने न केवल प्राइवेट वक्फ और पब्लिक वक्फ में वरन् धार्मिक उद्देश्यों और पुण्यार्थ उद्देश्यों में भी अन्तर पैदा कर दिया है।
उत्तर- (ii) विधि के सभी स्रोतों में विधि-विकास में विधायन को सबसे उपयुक्त समझा जाता है। समाज सुधार और विधि संशोधन का सबसे शक्तिशाली शस्त्र यही है, और विधायन की श्रेष्ठता विधि विकास के सभी तरीकों से इतना अधिक है कि विकसित सभ्यता वाले देश विधि-स्रोत के रूप में विधायन को ही महत्व देते हैं और शेष स्रोतों को भूतकाल के अवशेष के रूप में ही देखते हैं। विधायन न केवल नये विधि का स्रोत है वरन् इसके द्वारा उस विधि का निरसन (समाप्त) किया जा सकता है जो पहले से वर्तमान है और जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। जैसे- मुस्लिम विधि-ग्रन्थों के बहुत से प्रावधान जो गुलामों से सम्बन्धित हैं अब भारत में गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् 1983 ई० से ही निरर्थक हो चुके हैं।
जैसा कि कुरान में वर्णित है कि –
“सभी स्त्रियाँ जो विवाहिता हैं वे भी तुम्हारे लिए हराम हैं सिवाय उन स्त्रियों के जो तुम्हारी दासियाँ हैं।”
किन्तु इण्डियन स्लैबरी एक्ट, 1843 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर देने पर दासियों के साथ विवाह को भी समाप्त कर दिया गया है।
निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा मुस्लिम विधि में पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन हुए हैं-
(1) जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 – इस अधिनियम के लागू होने के पहले, जब कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन कर लेता था या धर्म का परित्याग करता था तो वह अपने परिवार में उत्तराधिकार में सम्पत्ति पाने के अधिकार से वंचित हो जाता था। किन्तु जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 ने मुस्लिम विधि के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और यह प्रावधान किया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने पर उत्तराधिकार या अन्य अधिकारों से वंचित न हो सकेगा। अतएव अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता प्रदान करता है कि बिना किसी अधिकार को खोये वह दूसरा धर्म ग्रहण कर सकता है।
(2) बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 1929 – जिस किसी लड़के या लड़की ने मुस्लिम विधि के अनुसार यौवनावस्था (Puberty ) प्राप्त कर लिया है तो वह स्वतन्त्र है, जिससे चाहे उससे अपना विवाह करे, और संरक्षक उसके कार्य में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते। किसी साक्ष्य के अभाव में यौवनावस्था की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है जब किसी व्यक्ति ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यौवनावस्था की उम्र से कम की दशा में संरक्षक लड़के या लड़की का विवाह कर सकते हैं। संरक्षक द्वारा किया गया विवाह वैध और मान्य होता है, हालांकि ऐसे विवाह का विखण्डन किया जा सकता है। बाल विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 में 1 अक्टूबर, 1978 के संशोधन के बाद लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है।
(3) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 – इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भी मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद का वाद दायर नहीं कर सकती थी। विवाह सम्बन्ध समाप्त करने का अधिकार पति को ही प्राप्त था। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के अंतर्गत कुछ आधारों पर मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर कर सकती है।
(4) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 – भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, यह अधिनियम विवाह करने का एक विशेष ढंग प्रावधानित करता है। यह एक सामान्य अधिनियम है जिसका लाभ जो लेना चाहें वे ले सकते हैं।
मुस्लिम विधि में कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी ऐसी गैर-मुस्लिम स्त्री से मान्य विवाह कर सकता है जो ईसाई या यहूदी हो, किन्तु मूर्तिपूजक या अग्निपूजक न हो। किन्तु कोई भी मुस्लिम स्त्री अपना विवाह किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से, चाहे वह पुरुष ईसाई, यहूदी, मूर्तिपूजक या अग्निपूजक ही क्यों न हो, नहीं कर सकती। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत कोई भी मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम स्त्री किसी गैर-मुस्लिम से विवाह कर सकते हैं और यह गैर-मुस्लिम हिन्दू मूर्तिपूजक या अग्निपूजक भी हो सकता है।
(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम पति, विवाह, विच्छेद के बाद केवल इद्दत अवधि तक ही भरण-पोषण करता है उसके बाद नहीं। किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 ने मुस्लिम विधि की उक्त अवधारणा को बदल दिया। चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्म निरपेक्ष विधि है अतः यह सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होती है और धारा 125 यह प्रावधान करती है कि विवाह विच्छेद के बाद यदि कोई स्त्री दूसरा विवाह नहीं करती है तो ऐसी अवस्था में पति भरण-पोषण के लिए दायी होगा अर्थात् यह उपबंध मुस्लिम विधि पर लागू होता है यानि मुस्लिम पति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार तलाकशुदा महिला को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण-पोषण देने के लिए दायी होगा। किन्तु शाहबानो बेगम के वाद के बाद संसद ने एक नया अधिनियम मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित कर मुस्लिम तलाकशुदा महिला को फिर पति से इद्दत अवधि तक ही भरण- पोषण का प्रावधान किया उसके बाद उनके भरण-पोषण का दायित्व उनके नजदीकी रिश्तेदारों एवं वक्फ बोर्ड के ऊपर डाल दिया गया।
प्रश्न 5. (i) मुस्लिम विधि के स्कूलों (विचारधारा सम्प्रदाय) के जन्म तथा विकास की संक्षेप में विवेचना कीजिए। शिया तथा सुन्नी स्कूलों के मध्य मुख्य अन्तर बताइए।
या
मुस्लिम विधि की दो प्रमुख शाखाओं के प्रमुख तत्व तथा उनके योगदान की चर्चा करें।
Discuss the origin and development of various schools of Muslim Law in brief. Point out the difference between Sunni and Shiya Schools.
OR
Discuss the main elements and the contribution of two Principal branches of Muslim Law.
(ii) मुस्लिम विधि की नवीनतम शाखा ‘अहमदिया’ के विषय में संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe in brief the subject of new branch Ahamadiya of Muslim Law.
उत्तर- (i) सन् 632 में अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद साहब मुस्लिम सम्प्रदाय के निर्विवाद सर्वोच्च नेता थे। मोहम्मद साहब ईश्वर के दूत के रूप में ईश्वरीय संदेश अपने लोगों को देते थे जो बिना तर्क तथा विवाद के स्वीकार होते थे, परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि मोहम्मद साहब को कोई पुत्र नहीं था। उनकी मृत्यु के समय उनकी एकमात्र पुत्री फातिमा ही जीवित थी। उत्तराधिकार के लिए विवाद के एक पक्ष का यह कथन था कि मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी उनके परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। अतः चूँकि अली, मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे तथा उनकी पुत्री फातिमा के पति थे, वही वैध उत्तराधिकारी माने गये। यह पक्षकार शियां सम्प्रदाय कहलाया। दूसरे पक्षकार का यह कथन था कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चयन मताधिकार द्वारा होना चाहिए। मोहम्मद साहब की जीवित सबसे छोटी पत्नी (विधवा) आयशा ने अपने पिता अबूबकर को (मुस्लिम सम्प्रदाय के नेता) मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी (खलीफा) के रूप में निर्वाचित करवा दिया। यह सम्प्रदाय सुन्नी सम्प्रदाय कहलाया।
निर्वाचित खलीफा अबू बकर दो वर्ष ही खलीफा रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् मोहम्मद साहब के शिष्य उमर खलीफा चुने गये। उमर की हत्या के पश्चात् उस्मान को खलीफा चुना गया। उस्मान भी बारह वर्ष तक खलीफा रहे और सन् 656 ई० में उनकी हत्या के पश्चात् अली जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे तथा उनकी पुत्री फातिमा के पति थे चौथे खलीफा निर्वाचित हुए। यह अली शियाओं द्वारा मोहम्मद साहब के परिवार के होने के आधार पर प्रथम खलीफा बनाये गये थे। इस प्रकार शिया लोग उत्तराधिकार के आधार पर अली को प्रथम खलीफा मानते थे परन्तु सुन्नी लोग निर्वाचन के आधार पर अली को अबूबकर, उमर तथा उस्मान के पश्चात् चौथा खलीफा मानते थे। शिया सम्प्रदाय के लोग अली को प्रथम खलीफा मानते थे तथा अबू बकर, उमर तथा उस्मान को वास्तविक उत्तराधिकारी न होने के कारण जबरन खलीफा पद प्राप्त करने वाले मानते थे। अली सिर्फ पाँच वर्ष तक खलीफा रहे उसके पश्चात् उनकी भी हत्या कर दी गई।
इस प्रकार स्पष्ट है कि नेता-पद या खलीफा पद के विवाद के कारण मुस्लिम सम्प्रदाय दो पृथक् वर्गों में विभक्त आ-एक वर्ग जो अली को पारिवारिक उत्तराधिकार के आधार मर प्रथम खलीफा मानता था, शिया कहलाया तथा दूसरा वर्ग जो अली को निर्वाचन के आधार पर चौथा खलीफा मानता था, सुन्नी कहलाया। यद्यपि इस विवाद को तेरह सौ वर्षों से अधिक व्यतीत हो चुके हैं परन्तु मुस्लिम सम्प्रदाय अली को दो पृथक् सम्प्रदायों (शिया तथा सुन्नी) में विभक्त होकर, उस विवाद को आज भी भूल नहीं पाये हैं। इस मतभेद का कारण धार्मिक कम, राजनैतिक अधिक था। ईरान शिया बहुल देश है। अन्य मुस्लिम देशों में सुन्नी बहुतायत में हैं।
(1) सुन्नी शाखा
सुन्नी सम्प्रदाय का उद्भव मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चुनाव (निर्वाचन मतदान) के आधार पर नियुक्त करने वालों से हुआ। ईरान को छोड़कर अन्य सभी मुस्लिम देशों में इसी शाखा के लोग बहुतायत में हैं। इसके विभिन्न उपसम्प्रदाय हैं- (1) हनको, (2) मलिकी, (3) शफी (4) हनवाली।
(1) हनफी (Hanafi)- इस उपशाखा या सम्प्रदाय के संस्थापक थे- नूमान। जिन्हें लोग आदर से हनीफ (वास्तविक धर्मपिता) कहते थे। नुमान या हनीफ ने इस्लाम तथा दैवी रहस्यवाद के पश्चात् विधिशास्त्र (फिक्ह) का अध्ययन किया। इन्होंने शिया सम्प्रदाय के कुछ इमामों तथा हदीस के विद्वान ऐशबाबी, कदादा तथा मालए मास से हदीसों का अध्ययन किया। हनीफ एक विद्वान व्यक्ति थे। बगदाद के सम्राट् अलमन्सूर ने अबू हनीफ को काजी- पद ग्रहण करने का निवेदन किया परन्तु अबू हनीफ ने इस पद को अस्वीकार कर दिया। बगदाद के सम्राट ने उन्हें कष्ट दिया तथा कैद में डाल दिया। कारागार में ही उनकी मृत्यु हो गयी। अबू हनीफ ने विधि के संहिताकरण (Codification) के लिए एक समिति बनाई, जिसे तीन वर्ष के परिश्रम के फलस्वरूप एक संहिता (Code) तैयार किया। अबू हनीफ का विधिशास्त्र का संग्रह ‘फिक-ए-अकबर’ में है। हनफी सम्प्रदाय के लोग मौखिक हदीसों पर विश्वास नहीं करते उनका विश्वास लिखित इज्मा पर अधिक है। अबू हनीफ व्यक्तिगत उपधारणा पर विश्वास नहीं करते थे। अबू हनीफ का विश्वास उदाहरण द्योतक उपधारणा (अनुमान) तथा विधिशास्त्रियों के अन्तःकरण पर अधिक था। उन्होंने साम्या के आधार पर इज्तिहाद नाम से एक विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रचलित किया। हनाफी सम्प्रदाय इज्मा तथा इज्तिहाद पर अधिक विश्वास करता था। हनाफी शाखा स्थानीय रीति-रिवाजों (Customs प्रथाओं) को मान्यता प्रदान करता था। उन्हें मौखिक हदीसों पर बहुत कम विश्वास था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा तुकीं में इस सम्प्रदाय को मानने वाले बहुतायत में हैं।
(2) मलिकी शाखा (Muliki Branch) – इस सम्प्रदाय या शाखा के प्रवर्तक मलिक-इब्न-अनास थे। मालिकी इब्न अनास मदीना में रहे तथा यहीं उन्होंने अपने उपदेश दिये। इनका विश्वास कुरान तथा हदीस पर आधारित विधिशास्त्र पर अधिक था। मालिक सम्प्रदाय के लोग हदीस में वर्तमान विरोध का हल इजमा की सहायता से करते हैं। मलिक ने एक ग्रन्थ में लिखा जिसका नाम मुवत्ता था। मुवत्ता का अर्थ है, रास्ते को सरल करना। मुवत्ता हदीसों का एक लघु संग्रह है। मालिकी सम्प्रदाय में परिवार के मुखिया की शक्ति शिशुओं तथा स्त्रियों पर अधिक होती है। इस सम्प्रदाय में विवाहिता स्त्री अपने पति की सम्पत्ति की सम्पूर्ण स्वामिनी नहीं होती। वह सम्पत्ति को पति की आज्ञा के बिना विक्रय, दान आदि नहीं कर सकती। वयस्क पुत्री तथा पुत्रियों पर भी पिता का नियंत्रण रहता है। चूँकि मालिकी सम्प्रदाय के शिक्षक न्यायाधीश तथा वकील रहें हैं अतः वे ऐसी ही बातें करते थे जो व्यावहारिक (Practical) हों। इस सम्प्रदाय के लोग रिवाज (प्रथा) को मान्यता देते हैं।
(3) शफी सम्प्रदाय (शाखा) – शफी के प्रवर्तक मोहम्मद इब्न-इदरीश-शफी थे। इनकी शिक्षा-दीक्षा मदीना में मालिकी शाखा के प्रवर्तक मलिक के अधीनस्थ तथा बगदाद में हनफी शाखा के प्रवर्तक हनाफी के अधीनस्थ हुई थी। इस कारण इस शाखा में मलिकी तथा हनाफी दोनों शाखाओं का समन्वय मिलता है। मोहम्मद इब्न इदरीश शफी इस्लाम धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने विधि सम्बन्धी अपने ज्ञान का निचोड़ अपनी पुस्तक रिसाला में प्रस्तुत किया। इस शाखा की प्रामाणिक पुस्तक इमाम नवाबी द्वारा लिखित पुस्तक मिनहाज है। इस शाखा के लोग रस्म-रिवाज (प्रथाओं) पर अधिक बल देते हैं। इस शाखा के समर्थक दक्षिणी मित्र, काहिरा, इन्डोनेशिया, मलेशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग हैं। भारत में बहुत कम अनुयायी बम्बई के कोकीन्स, मालाबार के भोपाल में हैं।
(4) हनबाली शाखा (Hanbali Branch)- इस शाखा के प्रवर्तक मोहम्मद इब्न इदरीस शफी के शिष्य अहमद इब्न हनबाल थे। हनबाली हदीसों पर विश्वास करता था। हनबाली अधिक कट्टर तथा प्रतिक्रियावादी था। इनबाली शाखा के अनुयायी सीरिया तथा फिलीस्तीन में पाये जाते हैं। अठारहवीं शताब्दी में वहाब नामक व्यक्ति ने इस विचारधारा में कुछ संशोधन किया तथा उसके समर्थक वहाबी (Wahabi) कहलाये। भारत में हनबाली सम्प्रदाय प्रचलित नहीं है।
(II) शिया शाखा (Shiya Branch)
जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को, उसके परिवार का कोई सदस्य है, ऐसा मानकर पैगम्बर की पुत्री फातिमा के पति तथा मोहम्मद साहब के चचेरे भाई अली को खलीफा माना, वे शिया कहलाये। शिया का शब्दिक अर्थ है- दल या पार्टी (Party)। शिया सम्प्रदाय के अनुसार अली मोहम्मद साहब के रिश्तेदार होने के कारण प्रथम खलीफा थे जबकि सुन्नी सम्प्रदाय के अनुसार निर्वाचन के माध्यम से चुने जाने के कारण अली को चौथा खलीफा मानते थे।
अली तथा पैगम्बर की पुत्री फातिमा के दो पुत्र थे- हसन तथा हुसैन। हसन बड़ा पुत्र था। वह संत स्वभाव का था। इसकी मृत्यु 669 ई० में जहर देने के कारण हुई। हसन की मृत्यु के पश्चात् अली का कनिष्ठ पुत्र हुसैन को तीसरा इमाम मानते हैं। हुसैन जब कर्बला के युद्ध में शहीद हो गये तो इस्लाम में एक नयी धार्मिक शाखा या सम्प्रदाय प्रारम्भ हुई, और शिया लोग इसी हुसैन के परिवार के समर्थक तथा अनुयायी हैं।
शिया सम्प्रदाय के अन्तर्गत तीन प्रमुख उपसम्प्रदाय हैं- (1) इसना अशारिया, (2) इस्माइलिया, (3) जैदिया।
(1) इसना अशारिया- भारत के अधिकांश शिया-सम्प्रदाय के लोग इसना अशारिया उपसम्प्रदाय (शाखा) के समर्थक तथा अनुयायी हैं। ये लोग अली, हसन, हुसैन, अली असगर, बाकिर, सादिक, काजिम, रजा, जावेद, अलहाजी, अल-असकरी तथा अलमुन्तजर नामक बारह इमामों को मानते हैं तथा उनके वंशज हैं।
ईरान के अधिसंख्य शिया इसी उपसम्प्रदाय को मानने वाले हैं। हमारे देश में इस उपशाखा के अनुयायी लखनऊ, रामपुर तथा हैदराबाद में हैं। इसना अशारिया उपशाखा के लोग सुन्नियों के निर्वाचित प्रथम तीन खलीफाओं- अबू बकर, उमर तथा उस्मान को खलीफा के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा अली के बारे में जो बातें सुन्नियों के हदीस में वर्णित हैं उन्हें भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि सुन्नियों की हदीसों में अली को अपने पूर्ववर्ती तीन खलीफाओं के सहायक के रूप में वर्णित किया गया है। इस सम्प्रदाय के लोगों के लिए इमाम की सत्ता ही सर्वोपरि है तथा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ही विधि स्रोत है।
(2) इस्माइलिया शाखा (Ismilia Branch) जफर अल-सादिक छठें इमाम थे। उनके दो पुत्रों में इस्माइल बड़े पुत्र थे जो अपने पिता के जीवन काल में. ही मर गये थे। इस उपशाखा के लोग इस्माइल को सातवाँ इमाम मानते हैं। इसलिए इस्माइलिया उपशाखा के अनुयायी सप्त इमामी (Sevencers) के रूप में भी जाने जाते हैं। इरमाइलिया शाखा के लोग इस्माइल को हो अल्लाह के बाद दूसरा स्थान देते हैं। इसना अशारिया उप सम्प्रदाय के लोग इस्माइल के बारे में अच्छा मत नहीं रखते। उनके अनुसार इस्माइल के बुरे आचरण के कारण इस्माइल के पिता ने इन्हें इमाम के पद से वंचित कर दिया था। मुसलमानों में खोजा तथा वोहरा (Khojas and Vohras) इस उपशाखा के अनुयायी हैं। उनकी प्रमुखता महाराष्ट्र तथा गुजरात में है।
(3) जैदिया उपशाखा (Jaidiya Branch) – इस शाखा के प्रवर्तक जैद थे। जैद मोहम्मद साहब के नाती तथा हुसैन के पौत्र थे। जैद उपशाखा को मानने वाले दक्षिणी अरब तथा यमन में पाये जाते हैं। जैदिया शाखा में शिया तथा सुन्नी विचारधारा का अद्भुत मिश्रण पाया जाता है। ये लोग खलीफा, अबू बकर तथा उमर को खलीफा को स्वीकार करते हैं परन्तु चूँकि खलीफा, उसमान मोहम्मद साहब के खानदान (कुरैश) के नहीं थे अतः खलीफा उस्मान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इनकी विचारधारा तथा इनका विधिशास्त्र मुता विवाह को घृणित मानने के कारण इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं देते।
मोताजिला सम्प्रदाय (Motazila sect) – 9वीं शताब्दी के आस-पास मैमन के शासन काल में मोताजिला सम्प्रदाय इस्लाम के एक विशिष्ट सम्प्रदाय के रूप में उभर सामने आया। इसके संस्थापक अता-उल-गजाली थे। ये अपने को शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं मानते। इस स्कूल के अनुयायियों की मान्यता है कि प्रत्येक नियम का आधार केवल कुरान हो सकता है। इस सम्प्रदाय का एक अतिविशिष्ट सिद्धान्त है जो किसी अन्य मुस्लिम सम्प्रदाय में नहीं है वह है “एक पत्नीत्व का नियम” जिसका बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है।
इस सम्प्रदाय के मानने वाले मुसलमान बहुत कम संख्या में हैं।
उप-सम्प्रदाय में परिवर्तन तथा उसका प्रभाव – सुन्नी तथा शिया शाखा एक ही सम्प्रदाय की शाखायें हैं, अतः शिया सम्प्रदाय या सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों को अपना सम्प्रदाय परिवर्तन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका प्रभाव यह होता है कि यदि सुन्नी, शिया या शिया सुन्नी सम्प्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसी तिथि से वह नवीन सम्प्रदाय या शाखा की वैयक्तिक विधि से शासित होने लगता है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि एक सम्प्रदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे सम्प्रदाय के व्यक्ति से विवाह कर लेने मात्र से इनका सम्प्रदाय परिवर्तन नहीं माना जाता, जैसे यदि एक सुन्नी लड़का, शिया लड़की से विवाह कर लेता है तो भी लड़का सुन्नी तथा लड़की शिया बनी रह सकती है तथा ऐसे विवाह से उत्पन्न लड़की (पुत्री) माता के सम्प्रदाय की तथा लड़का (पुत्र) पिता के सम्प्रदाय का सदस्य बना रहेगा। वयस्कता प्राप्त करने पर ऐसे विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को अपनी पसंदगी के सम्प्रदाय की सदस्यता ग्रहण करने की स्वतन्त्रता होगी।
मुस्लिम विधि की शिया तथा सुन्नी शाखाओं के मध्य विभिन्न विषयों पर अन्तर निम्न तालिका द्वारा प्रकट किया जा सकता है।
शिया एव सुन्नी विचारधारा में अन्तर
शिया-शाखा
1. विवाह
(1) शिया शाखा में मुता विवाह वैध है।
(2) शिया शाखा में ऐसी दो स्त्रियों को पत्नी बनाया जा सकता है जो चाची और भतीजी हों।
(3) शिया शाखा में जब हज के वस्त्र पहन लिए गये तो विवाह निषिद्ध माना जाता है।
(4) शिया शाखा में गैर-मुस्लिम स्त्री से सिर्फ मुता विवाह होना सम्भव है।
(5) शिया शाखा में निकाह की वैधता के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं है।
2. मेहर (Dower)
(1) शिया शाखा में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु अधिकतम सीमा 500 दिरहम (अरबी मुद्रा) निर्धारित है।
(2) शिया शाखा में मेहर की सम्पूर्ण राशि तुरन्त-देय मानी जाती है।
(3) शिया शाखा के अन्तर्गत विवाह के पक्षकारों द्वारा यह करार कि कोई मेहर देय नहीं होगी वयस्क तथा स्वस्थ मनःस्थिति की पत्नी द्वारा किया जा सकता है।
(4) शिया शाखा में मेहर की विषय वस्तु का करार के समय अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है।
3. तलाक या विवाह-विच्छेद
(1) शिया शाखा में तलाक मौखिक घोषणा द्वारा होना आवश्यक नहीं है परन्तु यदि पति बोलने में असमर्थ है तो यह घोषणा लिखित हो सकती है।
(2) शिया शाखा के अन्तर्गत नशे की हालत या मजाक में दिया गया तलाक शून्य होने के कारण प्रभावी नहीं होता।
(3) शिया शाखा के अन्तर्गत तलाक की घोषणा के समय गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है।
4. दान (हिया)
(1) शिया शाखा में आजीवन स्वत्व (Life title) का दान किया जा सकता है।
(2) शिया शाखा में सम्पत्ति के अविभाजित भाग का दान मान्य है, चाहे सम्पत्ति विभाजन योग्य हो या नहीं।
5. वसीयत
(1) शिया-शाखा के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के पक्ष में की गयी वसीयत उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना भी मान्य है, बशर्ते कि सम्पूर्ण सम्पदा के 1/3 से अधिक सम्पत्ति वसीयत के रूप में न दी गई हो।
(2) शिया शाखां के अन्तर्गत वसीयत- कर्त्ता के जीवन-काल में भी उत्तराधिकारी अपनी सहमति दे सकते हैं। यदि ऐसा है तो उत्तराधिकारियों की उस सहमति के पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है तथा 1/3 से अधिक की गई वसीयत मान्य होगी।
6. उत्तराधिकार (Inheritence)
(1) शिया शाखा में ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम सिर्फ मृतक के वस्त्र, घोड़ा, अंगूठी, तलवार तथा कुरान के सम्बन्ध में ही लागू होता है।
(2) शिया शाखा के अन्तर्गत प्रथम तथा दोनों वर्गों के उत्तराधिकारी साथ- साथ उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं।
(3) शिया शाखा के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त अंशतः लागू होता है।
(4) शिया शाखा के अन्तर्गत सन्तान विहीन विधवा अपने पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती।
(5) शिया शाखा के अन्तर्गत कोई व्यक्ति मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकार से तभी वंचित किया जा सकता है जब उसने हत्या जानबूझकर की हो।
सुन्नी-शाखा
1. विवाह
(1) सुन्नी शाखा में मुता विवाह वैध नहीं है।
(2) सुन्नी शाखा में चाची तथा भतीजी दोनों एक ही व्यक्ति की पत्नी नहीं हो सकतीं।
(3) सुन्नी सम्प्रदाय में हज के दौरान किया गया विवाह वैध है।
(4) सुन्नी शाखा में गैर इस्लामी औरत जो किताबिया (इसाई तथा यहूदी) है से विवाह वैध है।
(5) सुन्नी शाखा में विवाह (निकाह) की वैधता के लिए दो पुरुष गवाह या एक पुरुष तथा दो स्त्री गवाह की मौजूदगी आवश्यक है।
(6) सुन्नी शाखा में मान्य एवं शून्य विवाहों के अतिरिक्त अनियमित (Irregular) विवाह को भी मान्यता प्राप्त है।
2. मेहर (Dower)
(1) सुन्नी शाखा में न्यूनतम मेहर 10 दरहम निर्धारित है परन्तु मेहर की अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
(2) सुन्नी शाखा में मेहर का कुछ भाग तुरन्त-देय होता है तथा कुछ भाग स्थगित मेहर के रूप में होता है। कितना अंश तुरन्त-देय है तथा कितना स्थगित यह रीति-रिवाज के आधार पर निर्धारित होता है।
(3) सुन्नी शाखा के अन्तर्गत यह करार कि कोई मेहर देय नहीं होगी, शून्य होता है।
(4) सुन्नी शाखा में मेहर की विषय- वस्तु का विवाह या करार के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है।
3. तलाक या विवाह-विच्छेद
(1) सुन्नी शाखा में तलाक की घोषणा लिखित या मौखिक किसी रूप में भी हो सकती है।
(2) सुन्नी शाखा में नशे की हालत में या मजाक में, यहाँ तक कि यदि पति- पत्नी अभिनय कर रहे हैं, दिया गया तलाक मान्य तथा प्रभावी होता है।
(3) सुन्नी शाखा में तलाक की घोघणा के समय गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती।
4. दान (हिया)
(1) सुन्नी शाखा में आजीवन स्वत्व का दान नहीं हो सकता है। यदि होता है तो दान-ग्रहीता उस सम्पत्ति में पूर्ण-ग्रहीता उस सम्पत्ति में पूर्ण- स्वामित्व प्रदान करता है।
(2) जिस सम्पत्ति का विभाजन सम्भव नहीं है उसका अविभाज्य दान मान्य है परन्तु जिस सम्पत्ति का विभाजन सम्भव है उस सम्पत्ति का अविभाज्य भाग का दान अनियमित (Irregular) होता है।
5. वसीयत
(1) सुन्नी शाखा में किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत मान्य नहीं है। जब तक कि अन्य उत्तराधिकारीगण वसीयतकर्ता के मरणोपरान्त अपनी सहमति न दे दें।
(2) सुन्नी शाखा में किसी अजनबी के पक्ष में की गई वसीयत यदि सम्पत्ति के 1/3 से अधिक है तो तब तक मान्य नहीं है जब तक कि वसीयतकर्त्ता के मरणोपरान्त उत्तराधिकारीगण उसके लिये अपनी सहमति न दे दें।
6. उत्तराधिकार (Inheritence)
(1) सुन्नी शाखा में ज्येष्ठ पुत्राधिकार का नियम लागू नहीं होता ।
(2) सुन्नी शाखा में प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी दूसरे वर्ग को तथा दूसरे वर्ग के उत्तराधिकारी तीसरे वर्ग को अपवर्जित या बहिष्कृत करते हैं।
(3) सुन्नी शाखा के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू नहीं होता।
(4) सुन्नी शाखा के अन्तर्गत सन्तान- विहिन विधवा अपने पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती है।
(5) सुन्नी शाखा के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जानबूझकर या अनजाने में हत्या कर देता है तो वह मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।
उत्तर- (ii) मुस्लिम विधि की वैसे तो मुख्यतया दो ही शाखायें हैं पहला-सुन्नी शाखा, दूसरा-शिया शाखा किन्तु इसी क्रम में एक तीसरी नवीनतम शाखा अहमदिया-शाखा है। इस शाखा के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद अल-कादियानी थे जिनकी मृत्यु 1908 में हुई थी। उनकी मृत्यु के पूर्व ही उनके समर्थकों ने यह घोषणा की थी कि भारत में उनकी शाखा को एक पृथक मुस्लिम सम्प्रदाय माना जाय। अपने मत का प्रसार करने में अहमदिया लोग काफी हद तक सफल भी हुए। दक्षिण-पूर्व एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका में हजारों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। उनका यह दावा है कि उनके समर्थकों और अनुयायियों की संख्या 10 लाख से भी इस समय अधिक है।
अहमदिया-शाखा के विशेष सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-
(1) कुरान का कोई भी आयत निरस्त नहीं किया गया है, और न ही निरस्त किया जा सकता है। यदि कहीं एक आयत दूसरे आयत के विरोध में लागू हो तो वह टीकाकारों के दोषपूर्ण भाष्यों के कारण है।
(2) “जिहाद” या धर्म-प्रसार के लिए युद्ध गुजरे जमाने की वस्तु है, और धर्म के विषय में किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती निंदायोग्य है।
(3) यह कहना कि मोहम्मद साहब “पैगम्बरों की मुहर हैं, का यह अर्थ नहीं कि वे पैगम्बरों में अंतिम थे। मुहर केवल प्रामाणिकता का द्योतक है और यह बतलाता है कि मोहम्मद साहब में पैगम्बर के सभी गुण वर्तमान थे, किन्तु मोहम्मद साहब के पश्चात् भी कोई पैगम्बर हो सकते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा के पश्चात् भी यहूदियों के पैगम्बर अवतरित हुए।
(4) अन्य पैगम्बरों की तरह ईसा मसीह भी मर गये और वे सशरीर स्वर्गारूढ़ नहीं हुए।
(5) नरक भी सदैव बनी रहने वाली नहीं है।
(6) इस्लाम धर्म का परित्याग करने के कारण किसी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता।
(7) मजहबी आचरण में नई बातें चालू करना दोषपूर्ण है। सन्तों की पूजा ईश्वर (अल्लाह) की शक्ति और सत्ता पर संदेह व्यक्त करना है।
(8) धर्म स्रोत और विधि स्रोत के रूप में “इज्मा” या सहमति सामान्य रूप से ( पैगम्बर के सहयोगियों तक ही सीमित है।
(9) दैवी प्रेरणा सदैव मुसलमानों का विशेषाधिकार बनी रहेगी।
(10) मिर्जा गुलाम अहमद अल-कादियानी को मसीहा-महदी मानना धर्म की वस्तु है, और बिना इस स्वीकृति के धर्म अपूर्ण है।
(11) मजहब में आध्यात्मवाद का महत्व विधि वाद (legalism) से कहीं अधिक है। किसी अहमदिया के लिए किसी विशेष मजहब या विधि शाखा का होना आवश्यक नहीं है।
(12) कुरान या हदीस के अर्थान्वयन में या अर्थ लगाने में मध्यकालीन उलेमाओं का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है।
प्रश्न 6 (क) मुस्लिम विधि में विवाह (निकाह) से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक वैध विवाह के आवश्यक तत्वों की चर्चा करें।
What do you understand by marriage in muslim Law? Discuss the main elements of a valid marriage under Muslim Law.
(ख) मुस्लिम विधि में विवाह का क्या स्वरूप है? यह कहाँ तक संविदात्मक और संस्कारात्मक है? समीक्षा कीजिए।
Explain the form of Muslim Marriage. How for is it contractual and sacramental? Comment.
उत्तर (क)- निकाह (Marriage). – मुस्लिम विधि में विवाह के लिए निकाह (Nikah) शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘निकाह’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, योनि सम्बन्ध। निकाह शब्द से विवाह का तात्पर्य निकाला जाता है। प्रत्येक मुसलमान के लिए विवाह आवश्यक है। पैगम्बर मुहम्मद साहब ने विवाह करने का आदेश दिया है तथा उन अनुयायियों की निन्दा की है जो विवाह नहीं करते। जो व्यक्ति विवाह करता है वह सबाब (पुण्य) का कार्य करता है क्योंकि विवाह के द्वारा एक स्त्री को व्यभिचारिणी होने से बचाया जाता है तथा इससे सन्तान उत्पत्ति जैसा पुण्य कार्य करना सम्भव है।
सुन्नी शाखा में हेदाया के अनुसार विवाह सम्भोग, संतान-उत्पत्ति तथा उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए की गई संविदा है। किसी ऐसी स्त्री के साथ समागम (Cohabitation) जो उसकी पत्नी नहीं है, वर्जित तथा दण्डनीय है। इसके लिए हद्द के अन्तर्गत अधिकतम दण्ड का प्रावधान है।
मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं है। यह एक दीवानी संविदा है। न्यायमूर्ति महमूद ने, अब्दुल कादिर बनाम मुसम्मात सलीमा, (1886) 8 इला० 149 नामक बाद में कहा है: “मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संस्कार नहीं है अपितु एक दीवानी संविदा है तथा संविदा की भाँति निकाह में भी अधिकार तथा दायित्व तुरन्त तथा एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। पति द्वारा पत्नी को मेहर की अदायगी इसकी पूर्व-शर्त नहीं है।
मुस्लिम विधि के विद्वान, फैजी, मुल्ला तथा तैयबजी ने मुस्लिम विवाह को एक संविदा भी माना है। संविदा की भाँति मुस्लिम विवाह में भी प्रस्ताव (एजाब) की स्वीकृति (कबूल) होती है तथा प्रतिफल के रूप में मेहर का आदान-प्रदान होता है। मुस्लिम विवाह में मेहर आवश्यक है क्योंकि संविदा के लिए प्रतिफल अनिवार्य होता है और बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। यही बात सुबरुन्निसा बनाम सबद शेख, (1934) के वाद में भी कही गयी कि विवाह की संविदा में पत्नी सम्पत्ति और मेहर उसका मूल्य है।” इस प्रकार मुस्लिम विवाह में एक वैध संविदा की सभी औपचारिकताएं विद्यमान रहती हैं। परन्तु विवाह के लिए जहाँ पक्षकारों का बालिग (15 वर्ष) होना आवश्यक है वहीं संविदा के लिए सक्षमता की उम्र वयस्कता 18 वर्ष या 21 वर्ष है। अवयस्क का विवाह संरक्षक के माध्यम से कराया जा सकता है तथा ऐसा विवाह शून्य नहीं होगा जबकि अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होने के कारण उसका विधि की दृष्टि में कोई स्थान नहीं होता। संविदा के फलस्वरूप संविदा के पक्षकार किसी स्थिति को प्राप्त नहीं करते जबकि विवाह के पश्चात् एक पक्षकार पति तथा दूसरा पक्षकार पत्नी का पद ग्रहण कर लेता है। संविदा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार में माता-पिता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संविदा के अन्तर्गत संविदा का कोई पक्षकार संविदा भंग कर सकता है परन्तु मुस्लिम विवाह का सिर्फ एक पक्षकार (पति) ही विवाह भंग करने का अधिकार रखता है। इन कुछ अन्तरों के साथ मुस्लिम विवाह को एक संविदा के रूप में ही मान्यता प्राप्त है जबकि हिन्दू विवाह एक संस्कार है तथा प्रत्येक माता-पिता का पुनीत तथा धार्मिक कर्त्तव्य है कि वे अपनी पुत्री को सुयोग्य वर के हाथों में सौंपें। हिन्दू धर्म विवाह के पक्षकारों के लिए विवाह एक संस्कार है जिसके अभाव में जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं करता। माता-पिता के लिए यह धार्मिक अनुष्ठान है। हिन्दू विवाह में विवाह के पक्षकारों के प्रस्ताव या स्वीकृति का कोई महत्व नहीं है तथा न ही इसके लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता है।
एक वैध मुस्लिम विवाह के आवश्यक शर्तें- (1) यतिरेक पत्नी बाहुल्यम् (Single Husband and Plurality of wives). – मुस्लिम विवाह में बहुपत्नीत्व को तो मान्यता दी गई है, परन्तु बाहुपतित्व (Plurality of husbands) को व्यभिचार माना गया है।
कुरान के अनुसार एक मुसलमान के लिए अन्य पुरुष से विवाह स्त्री हराम है जब तक कि उस पुरुष ने उसे तलाक न दे दिया हो।
यदि कोई मुस्लिम स्त्री एक विवाह की निरन्तरता में किसी अन्य पुरुष से विवाह (निकाह) करती है तो ऐसा विवाह शून्य है तथा ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तान अवैध है। इतना ही नहीं, ऐसा करना व्यभिचार (जिना) माना जाता है तथा दण्डनीय है।
इस विषय में अहमद बख्श बनाम श्रीपति नाथू, ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 75 नामक वाद में यह प्रश्न उठा कि यदि एक मुस्लिम विवाहिता स्त्री धर्म-परिवर्तन कर प्रथम विवाह के रहते दूसरा विवाह करती है तो दूसरे विवाह का क्या प्रभाव होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा-धर्म-परिवर्तन से प्रथम विवाह समाप्त नहीं हो जाता। इस वाद में एक हिन्दू स्त्री विवाहिता होते हुए धर्म-परिवर्तन कर मुसलमान हो गई तथा इस धर्म-परिवर्तन के पश्चात् एक मुसलमान से विवाह किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा-धर्म-परिवर्तन के पश्चात् भी उस हिन्दू स्त्री का धर्म-परिवर्तन के पूर्व का विवाह समाप्त नहीं हुआ है तथा उसका धर्म-परिवर्तन के पश्चात् किया गया, विवाह शून्य था। अतः धर्म-परिवर्तन के पश्चात् किया गया दूसरा विवाह शून्य था तथा ऐसी सन्तान न तो प्रथम पिता, न ही दूसरे पिता की सम्पत्ति में ही उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती हैं।
मुस्लिम विधि बहुपतीत्व (Polygamy) को तो प्रतिबन्धित करती है परन्तु बहुपत्नीत्व (Polyandry) की आज्ञा प्रदान करती है तथा एक मुस्लिम पुरुष एक साथ अधिक से अधिक चार स्त्रियों से समागम कर सकता है। कुरान के अनुसार, “जो स्त्रियाँ तुम्हें पसन्द हों उनसे विवाह कर लो दो, तीन या चार।”
यदि कोई मुस्लिम पुरुष पाँचवीं स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसके परिणाम शिया तथा सुन्नी शाखा के अन्तर्गत भिन्न हैं। सुन्नी शाखा में पाँचवाँ विवाह अधिनियमित (फासिद : Irregular) होता है जबकि शिया शाखा के अन्तर्गत पंचम स्त्री से किया गया विवाह शून्य (Void: बातिल) होता है।
(2) विवाह के पक्षकारों के मध्य रक्त-सम्बन्ध (कराबत) (Consan- guinity) कुछ ऐसे सम्बन्ध हैं जिनके मध्य विवाह प्रतिबन्धित है। यदि ऐसे सम्बन्धों के मध्य विवाह सम्पन्न, होता है तो ऐसा विवाह बातिल (शून्य Void) होता है तथा इस विवाह से उत्पन्न सन्तान अवैध सन्तान मानी जाती है।
कुरान भी कहता है- “तुम्हारी माताएँ, पुत्रियर्थी, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बुआएँ, तुम्हारी मौसियाँ, तुम्हारी भतीजियाँ तथा भांजियाँ तुम्हारे लिए हराम म हैं।” इसके अतिरिक्त कुरान में कहा गया है कि जिस औरत के संग तुम्हारे पिता ने निकाह किया, उससे विवाह मत करो।
‘माता’ शब्द के अन्तर्गत माता, नानी, या दादी सम्मिलित हैं। परन्तु रूरी बनाम बाघसिंह, ए० आई० आर० 1935 लाहौर 23 नामक वाद में एक व्यक्ति ने अपने पिता के भाई (चाचा) की पत्नी से विवाह किया। यह विवाह वैध माना गया है तथा उससे उत्पन्न सन्तान को उत्तराधिकार प्रदान किया गया।
(ब) रक्त-सम्बन्ध के अतिरिक्त नजदीकी सम्बन्ध मुशारत (Affinity) – यदि पक्षकारों के मध्य रक्त-सम्बन्ध के अतिरिक्त किसी प्रकार नजदीकी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो ऐसे कतिपय सम्बन्धियों के मध्य विवाह प्रतिबन्धित है। जैसे पत्नी की माता, दादी, परदादी जितनी भी उच्च हो, पुत्र की पत्नी, पौत्र की पत्नी, पुत्री के पुत्र की पत्नी, जिस स्त्री के साथ सम्भोग हो चुका है, उसकी पुत्री, पौत्री या जितनी भी निम्न हो।
इस प्रकार का निकट सम्बन्ध कभी-कभी विवाह पात्र से स्थापित हो जाता है तो कभी- कभी सम्भोग के आधार पर। इस प्रकार पत्नी की माता (सास) से सम्बन्ध पत्नी से विवाह- मात्र से स्थापित हो जाता है, चाहे पत्नी से सम्भोग हुआ हो या नहीं। जैसे अपनी सास से मुस्लिम का विवाह प्रतिबन्धित है, चाहे पत्नी से सम्भोग हुआ हो या नहीं परन्तु पत्नी की पुत्री या पौत्री के साथ विवाह का प्रतिबन्ध तभी होता है जब पत्नी के साथ सम्भोग हुआ हो। इस प्रकार एक पुरुष ऐसी पत्नी की पुत्री से विवाह कर सकता जिसके साथ उसने सम्भोग नहीं किया है।
जमशेद अली बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०, (2004) रे० डि० 684 (उच्च न्यायालय) के मामले में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, श्वसुर के मृत्युपरान्त दामाद द्वारा अपनी सौतेली सास के साथ किया गया पुनर्विवाह वैध है न्यायालय ने कहा कि दामाद यदि अपनी सगी विधवा सास (जिसकी पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाहित हो) से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करे तो मुशारत (affinity) में आने के कारण विवाह शून्य होगा और वह विवाह पश्चात् मृत पति की सम्पत्ति से उत्तराधिकार का अधिकार खो देगी। उपरोक्त केस के तथ्य (facts) इस प्रकार से थे- मनसब अली का विवाह श्रीमती हकीमन (प्रथम पत्नी) से हुआ था और अपनी पुत्री श्रीमती हाजिरा को छोड़ते हुए 1950 में मर गया। श्रीमती हाजिरा का विवाह मुहम्मद नकी से हुआ और जमशेद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीमती हाजिरा की मृत्यु उपरान्त मुहम्मद नक्की ने अपने मृत श्वसुर की दूसरी विधवा पत्नी (सौतेली सास) श्रीमती खातून से विवाह कर लिया। प्रश्न उठा कि मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह वैध है या नहीं। माननीय न्यायालय ने मुल्ला की मोहम्मडन लॉ के पैरा 261 का आधार लेते हुए उत्तर दिया कि मुशारत या विवाह सम्बन्ध के आधार पर विवाह पूर्णतः वर्जित है। वे चार स्थितियाँ उपरोक्त प्रस्ताव में उल्लिखित हैं।
(स) धात्रेय (दूध) सम्बन्ध या रिज़ा (Fosterage) धात्रेय (Fosterage) सम्बन्ध का अर्थ है दूध का रिश्ता। यदि किन्हीं दो बच्चों ने एक ही स्त्री के स्तनों से दुग्ध पान किया है तो उनके मध्य धात्रेय (दूध) सम्बन्ध या रिजा स्थापित हो जाता है।
कुरान भी कहता है- “तुम्हारी मातायें जिन्होंने तुम्हें स्तन-पान कराया है, वे विवाह के प्रयोजन से तुम्हारे लिए हराम हैं।”
इस प्रतिबन्ध के पीछे यह तर्क है कि जो बच्चा किसी स्त्री का दूध पीता है वह अपनी खुराक उस स्त्री से प्रास करता है तथा ऐसे बच्चे का शरीर उस स्त्री के शरीर का अंश हो जाता है। यदि दो बच्चे एक ही स्त्री का स्तन पान करते हैं (दूध पीते हैं) तो उनके मध्य धात्रेय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा वह उस स्त्री का पति भी उस बच्चे का पिता हो जाता है जिसे उसकी पत्नी ने दूध पिलाया है यद्यपि कि उस स्त्री के स्तन में दूध उसके पति द्वारा उसे गर्भाधान किये जाने का परिणाम न था। इस प्रकार धात्रेय बच्चे यद्यपि रक्त-सम्बन्ध समझा जाता है। अतः धात्रेय सम्बन्ध में सम्पन्न विवाह शून्य (बातिल) होते हैं, किन्तु सुन्नी लोग कुछ अपवाद मानते हैं।
(3) समकालीन दो बहिनों के संग विवाह (Contemporaneous marriage with two sisters) कोई मुसलमान एक साथ दो सगी बहनों से विवाह नहीं कर सकता। कुरान के अनुसार “दो बहनों का एक साथ विवाह बन्धने में रखना भी तुम्हारे लिऐ हराम है।” हेदाया तथा फतवा -ए-आलमगीरी द्वारा इस प्रतिबन्ध का अर्थ लगाते हुए कहा गया है-किसी पुरुष के लिए यह वैध नहीं है कि वह किसी ऐसी दो औरतों से विवाह करे जो रक्त-सम्बन्ध, विवाह या धात्रेय सम्बन्ध से इस प्रकार सम्बन्धित हों कि उनमें यदि एक पुरुष होता तो विधितः उनका एक दूसरे से निकाह सम्भव न होता।
कलकत्ता उच्च न्यायालय का कसमस ऐजुन्निसा बनाम कुरीमुन्निसां, (1895) 23 कलकत्ता 130 नामक वाद इस बिन्दु पर प्रमुख वाद है। इस वाद में प्रश्न यह था कि यदि एक पुरुष प्रथम पत्नी के रहते उसकी सगी बहन के साथ विवाह करता है तो क्या यह विवाह वैध विवाह होगा।
इस वाद में गुलाम अली ने ऐजुन्निसा से विवाह किया। उसके रहते उसने उसकी छोटी बहन इज्जतुन्निसां से विवाह किया। इज्जतुन्निसां की एक पुत्री करीमुन्निसां के उत्तराधिकार को उसकी मौसी तथा उसकी सौतेली माँ एजुन्निसा ने चुनौती दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गुलाम अली का इज्जतुन्निसां के साथ विवाह प्रतिबन्धित होने के कारण शून्य (Void : बातिल) था तथा इस विवाह की सन्तान करीमुन्निसां को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था।
परन्तु अमीर अली ऐसे विवाह को अनियमित (फासिद: Irregular) मानते हैं तथा उनकी सन्तानों को वैध मानते हुए उन्हें उत्तराधिकार का हक देने के पक्ष में हैं। अधिकांश विधिशास्त्री इसी मत का समर्थन करते हैं तथा भारत में यह मत स्थापित हो चुका है कि दो सगी बहनों से किसी पुरुष के साथ एक साथ विवाह शून्य नहीं अपितु अनियमित (फ़ासिद) होगा तथा इसकी सन्तानें वैध होने के कारण इन्हें उत्तराधिकार प्राप्त होगा।
(4) किसी स्त्री के इद्दत काल में विवाह (Marriage with a woman undergoing the period of Iddat)- इद्दत की अवधि वह अवधि है जिसे हम विवाह-विच्छेद के पश्चात् ‘इंतजार की अवधि’ कह सकते हैं। यदि कोई मुस्लिम-विवाह या तो तलाक द्वारा या पति की मृत्यु के कारण विवाह विच्छेद हो जाता है तो विवाहिता स्त्री द्वारा कुछ निश्चित अवधि तक विवाह करने पर प्रतिबन्ध है। इस निश्चित अवधि को ‘इद्दत की अवधि’ (Iddat Period) कहा जाता है। यह प्रतिबन्ध इस जानकारी के लिए है कि क्या स्त्री अपने तलाकशुदा या मृतक पति से गर्भवती तो नहीं है जिससे कि होने वाले शिशु के पितृत्व का निर्धारण हो सके।
इद्दत की अवधि में पुनर्विवाह वर्जित है तथा इद्दत की अवधि में स्त्री के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व पति पर होता है।
इद्दत की अवधि तलाक द्वारा विवाह विच्छेद तथा पति की मृत्यु के कारण विवाह- विच्छेद के मामले में पृथक् पृथक् हैं।
यदि विवाह-विच्छेद तलाक द्वारा हुआ है तो यह अवधि विवाह के पश्चात् सम्भोग होने की दशा में तीन मासिक धर्मकाल की होगी तथा यदि तलाकशुदा स्त्री रजस्वला (हैज) नहीं है तो यह इद्दत की अवधि तीन चन्द्रमास तक विस्तारित होगी।
जैसा कि कहा गया है कि इद्दत की अवधि का प्रावधान इसका पता लगाने के लिए है कि क्या स्त्री विवाह-विच्छेद के पूर्व गर्भवती तो नहीं है। अतः यदि इद्दत की अवधि के दौरान यह विदित हो जाय कि स्त्री गर्भवती है तो इद्दत की अवधि शिशु के जन्म तक विस्तारित होती है।
इस प्रकार यदि स्त्री तलाकशुदा है तथा रजस्वला है तथा सम्भोग हुआ है तो इद्दत की अवधि तीन मासिक धर्मकाल तक या यदि तलाकशुदा स्त्री गर्भवती है तो यह अवधि शिशु के जन्म तक विस्तारित हो जाती है और यदि स्त्री रजस्वला नहीं है तो यह अवधि तीन चन्द्रमास तक होगी।
यदि विवाह के पश्चात् सम्भोग नहीं हुआ है तो तलाकशुदा स्त्री को इद्दत-काल मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी दशा में गर्भाधान का प्रश्न नहीं होता।
यदि विवाह-विच्छेद का कारण पति की मृत्यु है तो इद्दत काल चार मास दस दिन है, चाहे विवाह के पश्चात् सम्भोग हुआ हो या नहीं तथा यदि इस दौरान यह विदित हो जाय कि पत्नी गर्भवती है तो इद्दत-काल शिशु जन्म तक विस्तारित हो जाता है।
यदि विवाह-विच्छेद तलाक द्वारा हुआ है तथा विवाह के पश्चात् सम्भोग हुआ है तथा इद्दत की अवधि समाप्त होने से पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु की तिथि से नवीन इद्दत-काल प्रारम्भ हो जायगा। भले ही पति की मृत्यु विवाह-विच्छेद के कारण प्राप्त इद्दत-काल के पूरा होने के एक दिन पहले ही क्यों न हुई हो।
यदि विवाह-विच्छेद के पश्चात् प्राप्त इद्दत की अवधि पूरा होने के पूर्व ही शिशु का जन्म हो जाता है तो भी इद्दत की अवधि में कटौती नहीं होगी। भले ही शिशु चार, माह दस दिन के पूर्व ही उत्पन्न हो गया हो। तलाक के पश्चात् या पति की मृत्यु के पश्चात् इद्दत की अवधि आरम्भ हो जाती है चाहे तलाक या पति की मृत्यु की सूचना पत्नी को रही हो या नहीं।
इद्दत-काल का प्रतिबन्ध इस दशा में लागू नहीं होगा यदि किसी मुस्लिम पुरुष तथा मुस्लिम स्त्री ने विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1872 या 1954 के अन्तर्गत किया गया हो।
विशेष विवाह अधिनियम, 1872/1954 के अन्तर्गत कोई भी धर्म-मतावलम्बी विवाह कर सकता है। उसके लिए निम्न आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए :
(i) दोनों पक्षकारों के जीवन काल में पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए।
(ii) विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
(iii) विवाह के समय वर या वधू पागल या मूढ़ नहीं होना चाहिए।
(iv) विवाह के पक्षकारों के मध्य प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए।
(v) यदि विवाह भारत के बाहर सम्पन्न हुआ हो तो विवाह के पक्षकार भारत के नागरिक हों तथा उनका भारत में निवास होना चाहिए
(5) अपनी ही तलाकशुदा स्त्री से पुनर्विवाह (Remarriage with own divorced wife) यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है तथा यह तलाक तिबारा तलाक (Triple Talak) की भाँति प्रभावित हो जाता है तो वह पुरुष उसी तलाकशुदा स्त्री से तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक निम्न शर्तें पूरी नहीं होतीं :
(i) तलाकशुदा स्त्री इद्दत की अवधि व्यतीत न कर ले।
(ii) इद्दत की अवधि के पश्चात् तलाकशुदा स्त्री दूसरे मुस्लिम पुरुष से पुनर्विवाह न कर ले।
(iii) इस पुनर्विवाह के पश्चात् पति-पत्नी के मध्य सम्भोग न हो जाय।
(iv) द्वितीय पुरुष उस पत्नी को तलाक न दे दे।
(v) उस द्वितीय पुरुष द्वारा तलाक दिये जाने के पश्चात् वह स्त्री पुनः इद्दत की अवधि पूरी न कर ले।
कुरान में इस विषय में स्पष्ट प्रावधान है-
पति ने यदि पत्नी को तिबारा तलाक दे दिया है तो तत्पश्चात् जब तक वह स्त्री दूसरे पुरुष के साथ विवाह न कर ले तब तक वह स्त्री उस पति (पूर्व-पति) के लिए जायज(lawful) नहीं बन सकती। हाँ, यदि दूसरा पति (विवाह सम्भोग करके) उसको तलाक दे दे तो दोनों पर कुछ पाप नहीं कि एक दूसरे से विवाह बन्धन में बंध जायें। [कुरान 2-230.]
इस बिन्दु पर रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून, ए० आई० आर० 1932 प्रिवी कौंसिल 25 का वाद सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है-
इस वाद में गयासुद्दीन नामक सुन्नी मुसलमान ने अपनी पत्नी अनीसा खातून को तिबारा तलाक दिया। परन्तु वे तलाक के पश्चात् भी पति-पत्नी की भाँति रहने लगे। इससे उनके पाँच बच्चे हुए। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् उसके भाई रसीद अहमद ने इस आधार पर वाद किया कि तलाक के पश्चात् गयासुद्दीन तथा अनीसा खातून के मध्य सम्बन्ध अवैध था, अतः बच्चे जायज सन्तान न होने के कारण उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते।
प्रिवी काउन्सिल के अनुसार गयासुद्दीन तथा अनीसा खातून के मध्य तलाक अखण्डनीय था। चूँकि अनीसा खातून ने पर-पुरुष से विवाह नहीं किया था अतः उसके अपने पूर्व-पति से विवाह का अवरोध बरकरार था। अतः उनका पति-पत्नी की भाँति रहना नाजायज सम्बन्ध था, अतः इस विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध नहीं होने के कारण गयासुद्दीन की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते।
(6) विवाह के पक्षकारों की धार्मिक भिन्नता (Difference of Religion of Parties to the Marriage)- मुस्लिम धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ सुन्नी तथा शिया हैं तथा इनकी कई उपशाखाएँ हैं। सम्प्रदाय या उपसम्प्रदाय के आधार पर विवाह करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है अर्थात् एक सम्प्रदाय या उपसम्प्रदाय का पुरुष दूसरे मुस्लिम सम्प्रदाय या उपसम्प्रदाय की स्त्री से परस्पर आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।
यदि विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से भिन्न धर्म या सम्प्रदाय का है तो प्रावधान यह है कि एक मुस्लिम पुरुष चाहे सुन्नी हो या शिया एक किताबिया स्त्री से विवाह कर सकता है। किताबिया होने से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक आस्था मूर्ति या अग्नि में न होकर किताब (धर्मग्रन्थ) में हो। ईसाई तथा यहूदी लोगों की आस्था उनके धार्मिक ग्रन्थों में होती है। अतः ईसाई तथा यहूदी किताविया हैं।
हिन्दू किताबिया है या नहीं इस विषय पर कुछ निश्चित मत नहीं है क्योंकि हमारे देश में मुगल बादशाहों ने हिन्दू राजपूत स्त्रियों से विवाह किया था तथा उनकी सन्तानों ने वैध स्वीकार किये जाने के कारण उत्तराधिकार में शासन का अधिकार प्राप्त किया था। सम्राट् + जोधाबाई – जहाँगीर।
कोई भी मुस्लिम स्त्री किसी गैर-मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकती चाहे वह पुरुष किताबिया हो या मूर्तिपूजक या अग्निपूजक।
मुल्ला के अनुसार धार्मिक भिन्नता के प्रतिबन्ध के उल्लंघन में किया गया विवाह सिर्फ अनियमित (फासिद : Irregular) होता है तथा एक गैर-मुस्लिम पुरुष या स्त्री द्वारा किसी भी समय धर्म-परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने पर उक्त विवाह को नियमित किया जा सकता है।
फैजी महोदय उक्त बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक मुस्लिम पुरुष द्वारा गैर- मुस्लिम से किया गया विवाह अनियमित (फासिद) है। उसे उस स्त्री के धर्म-परिवर्तन कर मुस्लिम बनने पर नियमित किया जा सकता है। परन्तु यदि एक मुस्लिम महिला गैर-मुस्लिम से विवाह करती है तो यह विवाह शून्य (Void बातिल) विवाह होगा तथा उसे नियमित नहीं बनाया जा सकता। फैजी अपने मत के समर्थन में कुरान के द्वितीय समुल्लास की आयत 220 को उद्धृत करते हैं।
परन्तु आयत 221 इस मत के विपरीत है। यह आयत कहता है “मुशराकीन” (गैर- मुस्लिम) से विवाह न करो जब तक कि वे इस्लाम धर्म स्वीकार न कर लें और मुस्लिम स्त्रियों का विवाह मुशराकीन (गैर-मुस्लिम) से मत करो जब तक कि वे इस्लाम धर्म न स्वीकार कर लें।
इस प्रकार यह आयत मुस्लिम स्त्री या मुस्लिम पुरुष दोनों को मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने पर विवाह की इजाजत देकर पुरुष तथा स्त्री में इस सम्बन्ध में भेद नहीं करता। अतः दोनों दशाओं में विवाह के अनियमित या शून्य होने की कसौटी एक ही होनी चाहिए। ऐसा मुल्ला महोदय का मत है जो सही मत लगता है।
शिया पुरुष का गैर-मुस्लिम (बौद्ध) महिला के साथ विवाह– कोई मुस्लिम चाहे वह शिया हो या सुन्नी एक गैर-मुस्लिम महिला से विवाह नहीं कर सकता। परन्तु एक शिया किताबिया स्त्री से मुता विवाह कर सकता है तथा किताबिया में ईसाई तथा यहूदी के साथ पारसी भी आते हैं। परन्तु एक शिया एक गैर-मुस्लिम (बौद्ध) महिला से विवाह नहीं कर सकता जब तक कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार न कर ले। [अब्दुल रज्जाक बनाम आगा मोहम्मद, (1894) 21 आई० ए० 56]
एक मुस्लिम का ईसाई से विवाह – एक मुस्लिम पुरुष ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है जो किताबिया (ईसाई) है परन्तु एक मुस्लिम स्त्री ईसाई पुरुष, गैर-मुस्लिम से विवाह नहीं कर सकती।
(7) विवाह के पक्षकारों की सक्षमता (Capacity of Parties to Marriage) मुस्लिम विवाह के लिए मुस्लिम विधि में सक्षमता का आधार यौवनागमन (Puberty) है। मुस्लिम विधि में विवाह के लिए वयस्कता यौवनागम (Puberty) से प्राप्त होती है। यौवनागम (Puberty) की आयु 15 वर्ष है। कोई मुस्लिम युवक या युवती जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है विवाह करने के लिए सक्षम एवं स्वतन्त्र है तथा उसके संरक्षक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसी युवक तथा युवती ने यदि 15 वर्ष की आयु प्रास नहीं की है तो उसका विवाह संरक्षक के माध्यम से सम्पन्न कराया जा सकता है। पैगम्बर मोहम्मद साहब के विवाह के समय उनकी पत्नी आयशा की आयु सिर्फ 6 (छः) वर्ष ही थी।
एक अवयस्क व्यक्ति का संरक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा कराया गया विवाह शून्य होता है। संरक्षक द्वारा कराया गया विवाह वैध तो होता है परन्तु यौवनागम (Puberty) प्राप्त करने पर पति या पत्नी को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह विवाह को खण्डित कर दें।
ख्यारुल बुलूग (Option of Puberty: यौवनागम का विकल्प)- यदि किसी लड़के या लड़की का विवाह उसकी अवयस्कता के दौरान उसके संरक्षक (वली) द्वारा सम्पन्न कराया गया है तो बालिग (वयस्क) होने पर उसे यह विकल्प प्राप्त है कि वह उक्त विवाह का समर्थन करे या विखण्डन करे। युवक या युवती के इस विकल्प अधिकार को ख्यारुल-बुलूग (Option of Puberty) नाम दिया गया है।
मानव-जीवन की मुस्लिम विधि के अनुसार तीन अवस्थाएँ हैं- सगीर, सरीरी तथा बुलूग। इसी प्रकार हिन्दू विधि के अन्तर्गत मानव जीवन की चार अवस्थाएँ हैं- (1) ब्रह्मचर्य, (2) गृहस्थ, (3) वानप्रस्थ तथा (4) सन्यास ।
सगीर का प्रारम्भ जन्म से लेकर सात वर्ष तक की आयु का समय है। सरीरी की आयु सात वर्ष से 15 वर्ष तक है तथा बुलूग का आयु काल 15 वर्ष के पश्चात् से प्रारम्भ होता है। सगौर की अवस्था में किया गया विवाह शून्य होता है, चाहे वह संरक्षक के माध्यम से ही क्यों न किया गया हो। सरीरी की अवस्था में विवाह के पक्षकारों की सहमति का कोई महत्व नहीं होता तथा इस अवस्था में विवाह संरक्षक के माध्यम से सम्पन्न हो सकता है जो यौवनागमन की अवस्था (Puberty) प्राप्त होने पर विवाह के पक्षकार के विकल्प पर विखण्डित होता है। बुलूग की अवस्था में लड़का लड़की विवाह करने के लिए स्वतन्त्र माने जाते हैं तथा संरक्षक की अनुमति के बिना विवाह कर सकते हैं। ख्यारुल-बुलूग (Option of Puberty) का विकल्प प्रयोग होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं-
(1) विवाह 15 वर्ष की आयु (सगौर) में हुआ था।
(2) उसका विवाह पिता या किसी संरक्षक द्वारा सम्पन्न कराया गया था।
(3) ख्यारुल बुलूग (Option of Puberty) का प्रयोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किया गया था।
(4) यह कि विवाहोपरान्त सम्भोग नहीं हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि पन्द्रह वर्ष की आयु के पूर्व यदि सम्भोग हो भी जाता है तो भी ख्यारुल बुलूग (Option of Puberty यौवनागमन का विकल्प) समाप्त नहीं होता।
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 ने मुस्लिम विवाह विधि के आप्रखण्ड को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि इस अधिनियम ने इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किये गये विवाह को शून्य घोषित नहीं किया है, यद्यपि विवाह में भाग लेने वाले लोग दण्ड के दायी हैं।
(8) साक्षियों (Witnesses) की उपस्थिति (शहादत) (Presence of Vitnesses)- मुस्लिम विवाह एक संविदा है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति के साथ मेहर के रूप में प्रतिफल (विवाह का मूल्य) मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्त है।
मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा के अनुसार विवाह दो पुरुष या एक पुरुष तथा दो स्त्री द्वारा साक्षीकृत होना आवश्यक है जबकि शिया शाखा के अनुसार विवाह की वैधता के लिए विवाह का साक्षीकृत होना आवश्यक नहीं है।
सुन्नी विवाह को समर्थित करने वाले साक्षीगणों का बालिग (15 वर्ष की आयु प्राप्त) तथा मुस्लिम धर्मावलम्बी होना आवश्यक है। यद्यपि यदि एक मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है तो साक्षीगण गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ये साक्षी गूंगे तथा अन्धे तो हो सकते हैं परन्तु बहरे नहीं होने चाहिए। गवाह विवाह के पक्षकार के रिश्तेदार (Relatives) यहाँ तक कि उसके पुत्र भी हो सकते हैं।
गवाहों के लिए यह आवश्यक है कि उन्होंने विवाह के पक्षकारों के शब्दों को अवश्य सुना हो। यदि साक्षीगणों ने सिर्फ एक पक्षकार द्वारा उच्चारित किये गये शब्दों को ही सुना हो तो ऐसा विवाह वैध नहीं है। यहाँ तक कि पैगम्बर मोहम्मद साहब ने भी कहा कि “गवाहों के बिना विवाह नहीं हो सकता।” सुन्नी शाखा के मलिकी उपशाखा के अनुसार विवाह गवाहों के अभाव में भी वैध होते हैं। मुस्लिम विधि के विद्वानों ने गवाहों के अभाव में सम्पन्न विवाहों को अनियमित (फासिद: Irregular) माना है। दो गवाहों के प्राप्त होते ही इस प्रकार का विवाह नियमित (Regular) माना है। दो गवाहों के प्राप्त होते ही इस प्रकार का विवाह नियमित (Regular) होकर विधिपूर्ण हो जाता है।
(9) विवाह की औपचारिकताएँ (Formalities of Marriage)- मुस्लिम विवाह के लिए कोई विशेष अनुष्ठान होना आवश्यक नहीं है जबकि हिन्दू विवाह में विशेष अनुष्ठान आवश्यक है क्योंकि हिन्दू विवाह एक संस्कार है। मुस्लिम विवाह में ईसाई तथा मुस्लिम विवाह की भाँति किसी पुरोहित (मौलवी) का होना आवश्यक नहीं है।
मुस्लिम विवाह के लिए ‘प्रस्ताव तथा स्वीकार’ होना आवश्यक है। यदि विवाह के पक्षकार अस्वस्थ या अवयस्क हैं तो प्रस्ताव तथा स्वीकृति संरक्षकों के माध्यम से हो सकता है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति अरबी भाषा में हो या आवश्यक नहीं है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति विवाह के पक्षकारों की भाषा में इतने स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकले कि विवाह सम्पन्न हुआ था। विवाह के लिए प्रस्ताव तथा स्वीकृति भूतकाल या आज्ञात्मक (Imperative) रूप में होने चाहिए।
मुस्लिम विवाह के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही बैठक में हों। यदि ऐसा नहीं है तो विवाह अवैध होगा। [साहिब बीबी बनाम कमरुद्दीन (1911)]
विवाह की संविदा पत्र-व्यवहार द्वारा भी की जा सकती है। बशर्ते कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था पत्र पढ़कर गवाहों की उपस्थिति में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक निर्धारित प्रारूप में हो एक निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् औपचारिकता की उपधारणा (Presumption) की जा सकती है।
मुस्लिम विवाह के लिए सिर्फ एक औपचारिकता (Formality) आवश्यक है। वह है निकाह (Nikah)। यदि लड़की बिना किसी रस्म या औपचारिकता के पति को सौंप दी गई हो तो निकाह द्वारा उत्पन्न सम्बन्धों पर कोई असर नहीं पड़ता है।
उत्तर (ख)- मुस्लिम विधि में विवाह के लिए निकाह (Nikah) शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘निकाह’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, योनि-सम्बन्ध। निकाह शब्द से विवाह का तात्पर्य निकाला जाता है। प्रत्येक मुसलमान के लिए विवाह आवश्यक है। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने विवाह करने का आदेश दिया है तथा उन अनुयायियों की निन्दा की है जो विवाह नहीं करते। जो व्यक्ति विवाह करता है वह सबाब (पुण्य) का कार्य करता है क्योंकि विवाह के द्वारा एक स्त्री को व्यभिचारिणी होने से बचाया जाता है तथा इससे सन्तान उत्पत्ति जैसा पुण्य कार्य करना सम्भव है।
सुन्नी शाखा में हेदाया के अनुसार विवाह सम्भोग, संतान उत्पत्ति तथा उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए की गई संविदा है। किसी ऐसी स्त्री के साथ समागम (Cohabitation) जो उसकी पत्नी नहीं है, वर्जित तथा दण्डनीय है। इसके लिए हद्द के अन्तर्गत अधिकतम दण्ड का प्रावधान है।
मुस्लिम विवाह एक संस्कार नहीं है। यह एक दीवानी संविदा है। न्यायमूर्ति महमूद ने, अब्दुल कादिर बनाम मुसम्मात सलीमा, (1886) 8 इला० 149 नामक वाद में कहा है : “मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संस्कार नहीं है अपितु एक दीवानी संविदा है तथा संविदा की भाँति निकाह में ही अधिकार तथा दायित्व तुरन्त तथा एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। पति द्वारा पत्नी को मेहर की अदायगी इसकी पूर्व-शर्त नहीं है।
मुस्लिम विधि के विद्वान् फैजी, मुल्ला तथा तैयबजी ने भी मुस्लिम विवाह को एक संविदा ही माता है। संविदा की भाँति मुस्लिम विवाह में भी प्रस्ताव (एजाब) की स्वीकृति (कबूल) होती है तथा प्रतिफल के रूप में मेहर का आदान-प्रदान होता है। मुस्लिम विवाह में मेहर आवश्यक है क्योंकि संविदा के लिए प्रतिफल अनिवार्य होता है और बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। यही बात सुबरुन्निसा बनाम सबद शेख, (1934) के वाद में भी कही गयी कि विवाह की संविदा में पत्नी सम्पत्ति और मेहर उसका मूल्य है।” इस प्रकार मुस्लिम विवाह में एक वैध संविदा की सभी औपचारिकताएँ विद्यमान रहती हैं। परन्तु विवाह के लिए जहाँ पक्षकारों का बालिग (15 वर्ष) होना आवश्यक है वहीं संविदा के लिए सक्षमतां की उम्र वयस्कता 18 वर्ष या 21 वर्ष है। अवयस्क का विवाह संरक्षक के माध्यम से कराया जा सकता है तथा ऐसा विवाह शून्य नहीं होगा जबकि अवयस्क द्वारा की गई संविदां शून्य होने के कारण उसका विधि की दृष्टि में कोई स्थान नहीं होता। संविदा के फलस्वरूप संविदा के पक्षकार किसी स्थिति को प्राप्त नहीं करते जबकि विवाह के पश्चात् एक पक्षकार पति तथा दूसरा पक्षकार पानी का पद ग्रहण कर लेता है। संविदा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता जबकि विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न सन्तानों का उत्तराधिकार में माता-पिता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संविदा के अन्तर्गत संविदा का कोई पक्षकार संविदा भंग कर सकता है परन्तु मुस्लिम विवाह का सिर्फ एक पक्षकार (पति) ही विवाह भंग करने का अधिकार रखता है। इन कुछ अन्तरों के साथ मुस्लिम विवाह को एक संविदा के रूप में ही मान्यता प्राप्त है जबकि हिन्दू विवाह एक संस्कार है तथा प्रत्येक माता-पिता का पुनीत ताश धार्मिक कर्तव्य है कि वे अपने पुत्री कौ सुयोग्य वर के हाथों में सौंपें। हिन्दू धर्म विवाह के पक्षकारों के लिए विवाह एक संस्कार है जिसके अभाव में जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं करता। माता-पिता के लिए यह धार्मिक अनुष्ठान है। हिन्दू विवाह में विवाह के पक्षकारों के प्रस्ताव या स्वीकृति का कोई महत्व नहीं है तथा न ही इसके लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता है।
प्रश्न 7. (i) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत सहीड, फासिद तथा बातिल विवाहों से आप क्या समझाते हैं तथा इनके बीच क्या अंतर है?
Discuss the difference between Sahih (Valid) and Fasid (Void) marriages under Muslim Law and what is the difference among them?
(ii) मुता विवाह से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तों का ( उल्लेख कीजिए। ऐसे विवाह के के ि विधिक परिणाम भी स्पष्ट करें।
What do you understand by Muta Marriage? Discuss its essentials. Explain legal incidents of its Marriage.
उत्तर- (i) सहीह (Valid), फासिद (Irregular अनियमित) तथा शून्य (Void: बातिल) मुस्लिम विवाह –
(1) सहीह या नियमित विवाह (Valid or Regular Marriage) – ऐसा त्रुटिहीन विवाह जिसमें विवाह की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होती हैं सहीह विवाह कहलाता है। इस विवाह में विवाह के सम्बन्ध में निषेध (प्रतिबन्ध) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे विवाह रक्त-सम्बन्ध या धात्रेय सम्बन्ध के अंतर्गत न हो। विवाह (सगौर) सात वर्ष से कम आयु में सम्पन्न नहीं हुआ है, विवाह गर्भ छिपाकर न किया गया हो।
सहीह विवाह के लिए आवश्यक शर्तें- सहीह (वैध) विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है-
(i) विवाह के एक पक्षकार ने विवाह का प्रस्ताव किया हो और दूसरे पक्षकार ने उसे स्वीकार किया हो।
(ii) दोनों पक्षकार विवाह के लिए सक्षम हों तथा विवाह के लिए स्वतंत्र सम्मति दी हो।
(iii) प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही बैठक में हुई हो तथा यह सक्षम गवाहों के समक्ष हुआ हो।
(iv) विवाह के पक्षकार रक्त सम्बन्ध, विवाह सम्बन्ध, या धात्रेय सम्बन्ध के अन्तर्गत न आते हों।
सहीह या नियमित विवाह के परिणाम- फतवा-ए-आलमगीरी के अनुसार एक सहीह विवाह के निम्न परिणाम होते हैं-
(1) विवाह के पक्षकार आज्ञापित रीति से समागम (मैथुन) के हकदार हो जाते हैं। पति को यह अधिकार होता है कि पत्नी के स्वास्थ्य या शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए जब और जहाँ चाहे पत्नी से सम्भोग की माँग करें।
(2) पति को पत्नी की गतिविधियों पर उचित प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अन्तर्गत पति किसी अन्य पुरुष से मिलने या बात करने पर पत्नी को प्रतिबन्धित कर सकता है।
(3) सहीह विवाह के अन्तर्गत पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार हो जाती है।
(4) पत्नी विवाह के समय निर्धारित मेहर (Dower) प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है।
(5) सहीह विवाह की उत्पन्न सन्तानें जायज सन्तानें मानी जाती हैं तथा पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती हैं।
(6) पति की मृत्यु पर पत्नी को भी उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है।
(7) पति की मृत्यु या तलाक पर पत्नी इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य हो जाती है।
(2) अनियमित (Irregular) या फासिद विवाह- मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह के निषिद्ध अस्थायी प्रतिबन्ध के उल्लंघन में सम्पन्न विवाह अनियमित या फासिद विवाह कहलाता है। अनियमित विवाह की विशेषता यह है कि ऐसा विवाह कुछ प्रयत्न करने पर नियमित हो जाता है या कुछ समय पश्चात् प्रतिबन्ध दूर होने पर अनियमित विवाह नियमित हो जाता है।
उदाहरण के रूप में एक मुसलमान पुरुष एक साथ दो सगी बहनों से विवाह नहीं कर सकता, साथ-साथ दो सगी बहनों से किया गया विवाह अनियमित है। (मुसलमान एक साथ चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है।) यदि एक मुसलमान पुरुष दो बहिनों में से एक बहिन को तलाक दे देता है या एक बहिन मर जाती है तो उक्त अनियमित विवाह नियमित बन जायेगा।
अनियमित विवाहों के निम्नलिखित उदाहरण हैं-
(1) चार पत्नियों के रहते हुए, पाँचवीं स्त्री से किया गया विवाह।
(2) साक्षियों (गवाहों) के अभाव में किया गया विवाह।
(3) ऐसी स्त्री जो इद्दत-काल का पालन कर रही है, उससे किया गया विवाह।
(4) धार्मिक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया गया विवाह।
(5) एक साथ दो सगी बहनों से किया गया विवाह।
अनियमित विवाह के द्वारा स्थगित सम्बन्ध किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए न तो तलाक की आवश्यकता होती है और न ही विवाह विच्छेद की न्यायिक आज्ञमि (Judicial Decree)। यद्यपि अनियमित विवाह से उत्पन्न सन्तानों की पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है, परन्तु विवाह के पक्षकार पति-पत्नी को पारस्परिक उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता।
यदि अनियमित विवाह के पश्चात् सम्भोग हो जाता है तो पत्नी मेहर पाने की अधिकारिणी हो जाती है। अनियमित विवाह में पति की मृत्यु या तलाक के परिणामस्वरूप विवाह-विच्छेद होने पर इद्दत की अवधि सिर्फ तीन मासिक धर्म-मास तक ही होती है तथा पत्नी इद्दत काल में ही भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होती। इस प्रकार अनियमित विवाह में सम्भोग न होने तक विवाह का कोई विधिक परिणाम नहीं होता। हनाफी विधि में अनियमित विवाह के अन्तर्गत उत्पन्न सन्तान अपनी माता से उत्तराधिकार प्राप्त करेगी तथा सम्भोग के पश्चात् उत्पन्न सन्तान के लिये पितृत्व तथा धर्मजत्व का वहीं परिणाम होता है जो नियमित विवाह का।
रसीद अहमद बनाम अनीसा खातून, (1931) 59 आई० ए० 21 के मामले में कहा गया है कि वह विवाह शून्य विवाह की श्रेणी में आता है जो किसी ऐसी स्त्री से किया गया हो जिसका पति जिन्दा हो और उसका विवाह विच्छेद न हुआ हो अथवा अपनी ही तलाक दी हुई स्त्री से विवाह हुआ हो अथवा विवाह के लिए निर्धारित प्रतिबन्धों का निषेध हुआ हो।
(3) शून्य (Void) या बातिल विवाह – मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह के लिए निर्धारित स्थायी प्रतिबन्ध के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य या बातिल (Batil) विवाह होता है। इस वर्ग के विवाह का कोई भी विधिक परिणाम नहीं होता। इससे उत्पन्न सन्तानें अवैध (नाजायज) या दागी होती हैं। उन्हें अभिस्वीकृति द्वारा भी वैध नहीं बनाया जा सकता। केवल सम्भोग होने की स्थिति में मेहर प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है।
शून्य या बातिल विवाह के पक्षकार (पति या पत्नी) पारस्परिक अधिकार या दायित्व प्राप्त नहीं करते। विवाह के पक्षकार बिना विवाह विच्छेद या बिना विवाह-विच्छेद की न्यायिक आज्ञति (Judicial decree) प्राप्त किये अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह कर सकते हैं। शून्य विवाह की पत्नी भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती। उसे पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार भी प्राप्त नहीं होता।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा शून्य घोषित विवाह से उत्पन्न सन्तानें वैध होती हैं। परन्तु मुस्लिम विधि के अन्तर्गत शून्य विवाह से उत्पन्न सन्तान नाजायज या हरामी होती हैं। इन सन्तानों को वैधता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
शून्य या बातिल विवाह के कुछ उदाहरण निम्न हैं-
(1) विवाहित स्त्री के साथ (बिना तलाक लिए) किया गया विवाह जिसकी एक प्रक्रिया है।
(2) रक्त सम्बन्ध (Blood Relation) के अन्तर्गत किया गया विवाह।
(3) विवाह से सम्बन्धित स्त्री (सास) के साथ किया गया विवाह।
(4) धात्रेय सम्बन्ध (Fosterage Relation) के उल्लंघन में किया गया विवाह।
(5) अपनी ही तलाकशुदा स्त्री से बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाये किया गया विवाह।
वैध, अनियमित तथा शून्य विवाह में अन्तर
वैध विवाह (सहीह)
(1) वैध विवाह वह होता है जिसमें विवाह की सभी शर्तें पूरी होती हैं।
(2) वैध विवाह को नियमित करने की आवश्यकता नहीं होती।
(3) वैध विवाह की सन्तानें जायज होती हैं।
(4) वैध विवाह की सन्तानें पिता की तथा माता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं।
(5) वैध विवाह के पक्षकार पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व उत्पन्न करते हैं।
अनियमित विवाह (फासिद)
(1) अनियमित विवाह अस्थायी प्रतिबन्ध के – उल्लंघन में किया गया विवाह है।
(2) अनियमित विवाह अस्थायी प्रतिबन्ध के दूर हो जाने पर नियमित हो जाता है।
(3) अनियमित विवाह की सन्तानें जायज होती हैं।
(4) अनियमित विवाह की सन्तानें माता-पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं।
(5) अनियिमित विवाह के पक्षकार विवाह के नियमित होने पर पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व धारण करते हैं।
शून्य विवाह (बातिल)
(1) शून्य विवाह प्रतिबन्धित विवाह है जहाँ प्रतिबन्ध स्थायी होता है।
(2) शून्य विवाह का विधिक अस्तित्व नहीं होता है। अतः उसे किसी भी प्रकार वैधता नहीं प्रदान की जा सकती ।
(3) शून्य विवाह की सन्तानें हरामी होती हैं।
(4) शून्य विवाह की सन्तानों को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता।
(5) बातिल या शून्य विवाह चूँकि विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन है। अतः विवाह के पक्षकार पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व को धारण नहीं करते क्योंकि इस विवाह को किसी भी स्तर से वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है।
उत्तर- (ii) मुस्लिम विधि में मुख्यतः दो सम्प्रदाय हैं। पहला शिया सम्प्रदाय एवं दूसरा सुन्नी सम्प्रदाय। मुता विवाह केवल शिया सम्प्रदाय में प्रचलित है। सुन्नी सम्प्रदाय मुता विवाह को मान्यता नहीं प्रदान करता है। कोई भी शिया मुस्लिम सीमित काल के लिए विवाह-संविदा कर सकता है। यह सीमित समय कुछ वर्ष, मास, दिन या दिन का कोई भाग भी हो सकता है। ऐसे अस्थायी विवाह को मुता सम्बन्ध या अस्थायी विवाह कहा जाता है। “मुता” शब्द का शब्दिक अर्थ होता है- आनन्द’ और ‘विधि’ में लाक्षणिक भाव में इसका अर्थ होता है-आनन्दार्थ विवाह। अर्थात् केवल शिया सम्प्रदाय में ही सीमित समय के लिए विवाह या अस्थायी विवाह या मुता विवाह हो सकता है, सुन्नी सम्प्रदाय में नहीं क्योंकि सुन्नी सम्प्रदाय के अनुसार विवाह की संविदा की अवधि सीमित नहीं होनी चाहिए और विवाह के प्रस्ताव (एजाब) और स्वीकृति (कबूल) के समय में प्रयुक्त शब्द-समूह ऐसे होने चाहिए जो तात्कालिक और स्थायी सम्बन्ध बोध करावें। अतएव सुन्नी विधि के अंतर्गत सीमित समय के लिए किया गया विवाह शून्य होता है।
मुसम्मात सरवर आरा बनाम बहादुर अली खाँ आ० ३० रि० 1934 अवध 152 के मामले में न्यायालय ने कहा कि मुता सम्बन्ध में ‘चार पत्नियों की संख्या को सीमा’ लागू नहीं होती इस कारण शिया-सम्प्रदाय के नवाबों और सामन्तों ने पंचम और षष्ठ पत्नी को मुता रूप में ग्रहण किया।
वर्तमान समय में मुता-सम्बन्ध का प्रचलन बहुत ही कम है और कुछ ही कट्टरपंथी शिया लोगों द्वारा ही ऐसा अस्थाई विवाह किया जाता है। ईरान व ईराक में इसे विधिक वेश्यावृत्ति कहा जाता है।
मुता-विवाह के आवश्यक तत्व – मुता विवाह के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं- (1) सहवास की अवधि निश्चित होनी चाहिए, और यह उस समय निश्चित हो जब मुता-सम्बन्ध की संविदा की जाय,
(2) कुछ मेहर अवश्य ही उल्लिखित या निश्चित हो।
जब मुता-विवाह की अवधि और मेहर निश्चित की गई हो तो विवाह संविदा मान्य और वैध होती है। जिन मामलों में समय तो निश्चित किया गया है किन्तु मेहर निश्चित नहीं की गई है तो मुता विवाह को संविदा शून्य होगी। किन्तु जहाँ मेहर तो निश्चित की गई है किन्तु अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो वहाँ मुता विवाह तो शून्य होगा किन्तु ऐसा मुता- विवाह, स्थायी विवाह में परिवर्तित हो जायेगा।
एस० ए० हुसैन बनाम रजम्मा, ए० आई० आर० 1977 ए० पी० 154 के मामले में हबीबुल्ला नामक एक शिया पुरुष में और रजम्मा नामक एक हिन्दू स्त्री में प्रेम हो गया। रजम्मा इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई और तत्पश्चात् हबीबुल्ला ने रजम्मा से मुता विवाह किया।
हबीबुल्ला की मृत्यु पर रजम्मा विधवा की हैसियत से हबीबुल्ला की सम्पत्ति पर काबिज बतौर उत्तराधिकारिणी बनी। मृतक के सगे भाई एस० ए० हुसैन ने रजम्मा के सम्पत्ति प्राप्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि चूँकि रजम्मा मृतक हबीबुल्ला की मुताई पत्नी थी और मुताई पत्नी के पति के सम्पदा के उत्तराधिकार का हक नहीं होता, इस कारण रजम्मा को उत्तराधिकार में कुछ भी पाने का हक नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। अपील में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि यद्यपि इस विवाह में “मुता” शब्द का प्रयोग किया गया था, किन्तु चूँकि इसकी अवधि निश्चित नहीं थी, इसलिए यह विवाह निकाह माना जायेगा। निकाह में विधवा को मृत पति का उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः रजम्मा मृतक की विधवा की हैसियत से सम्पदा पाने की हकदार है।
मुता-विवाह के विधिक परिणाम मुता-संविदा के मान्य होने के विधिक परिणाम निम्नलिखित होते हैं-
(1) पक्षकारों में मैथुन कार्य विधिपूर्ण हो जाता है।
(2) मुता-सम्बन्ध के बने रहने के दौरान पैदा हुई या गर्भस्थित संतानें वैध होती हैं और वे दोनों माता-पिता से उत्तराधिकार पाने की हकदार होते हैं।
(3) विवाह के पक्षकारों को उत्तराधिकार प्राप्ति के पारस्परिक अधिकार नहीं होते हैं। किन्तु ऐसे अधिकार संविदा द्वारा सृजित किये जा सकते हैं या मुता सम्बन्ध की संविदा में तामिल किये जा सकते हैं।
(4) अवधि की समाप्ति पर मुता विवाह सम्बन्ध स्वतः विघटित हो जाता है। मुता- विवाह के सम्बन्ध में तलाक देने का अधिकार पति को प्राप्त नहीं होता है, किन्तु अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय भी पति शेष अवधि का दान पत्नी के पक्ष में कर सकता है।
इसी परिप्रेक्ष्य में अमौर अली ने अपनी पुस्तक मोहम्मडन लॉ में कहा है कि ऋणकतों को उसके ऋणों से उन्मुक्त करने के लिये ऋणकर्ता की सहमति आवश्यक नहीं होती पत्नी मुता-सम्बन्ध में केवल ऋणकर्ता (Debtor) है और पति है ऋणदाता (Creditor) और इस कारण पति मुता-सम्बन्ध की अवधि या उसके किसी भाग का त्याग मुताई पत्नी की सहमति बिना भी कर सकता है।
अतः यह स्पष्ट है कि मुता विवाह में तलाक सम्भव नहीं है किन्तु अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय पति शेष अवधि का दान पत्नी के पक्ष में कर सकता है। ऐसे दान को ‘हिबा-ए-मुद्दत’ कहते हैं। कमर कादर बनाम लुड्डन साहिबा, (1886) 14 कल० 216 के मामले में पक्षकार इसना अशारिया शिया सम्प्रदाय के थे। कमर कादर नामक व्यक्ति ने लुड्डन साहिबा नामक अविवाहित युवती से मुता रूप में पचास वर्ष के लिए विवाह संविदा की। इस बात के लिए सहमति थी कि पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार होगी। इस विवाह का सम्भोग भी हुआ। किन्तु विवाह के कुछ सप्ताह के पश्चात् ही कमर कादर ने उसे छोड़ दिया और जब लुड्डन साहिबा ने भरण-पोषण का वाद चलाया तो प्रतिवादी कमर कादर ने अभिकथन किया कि उसने मुता-सम्बन्ध मात्र 5/2 माह के लिए स्थापित किया था।
परीक्षण न्यायालय ने कमर कादिर की बात गलत पायी अतएव Cr.P.C. की धारा-125 के तहत उन्हें आदेश दिया कि वे मुताई पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करें। इसके बाद कमर कादिर ने घोषणात्मक वाद दायर करके कहा कि उसने ‘अवशेष अवधि का दान’ कर दिया है अतः विवाह विघटित हो गया और वह भरण-पोषण का दायी नहीं होगा इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मुता-सम्बन्ध में पति तलाक का इस्तेमाल नहीं कर सकता किन्तु अवशेष अवधि का दान या त्याग (हिबा-ए-मुद्दत) करके विवाह-सम्बन्ध खत्म कर सकता है।
(5) यदि विवाह सम्भोग नहीं हुआ है तो पत्नी निश्चित मेहर की आधी धनराशि ही पाने की अधिकारी होगी।