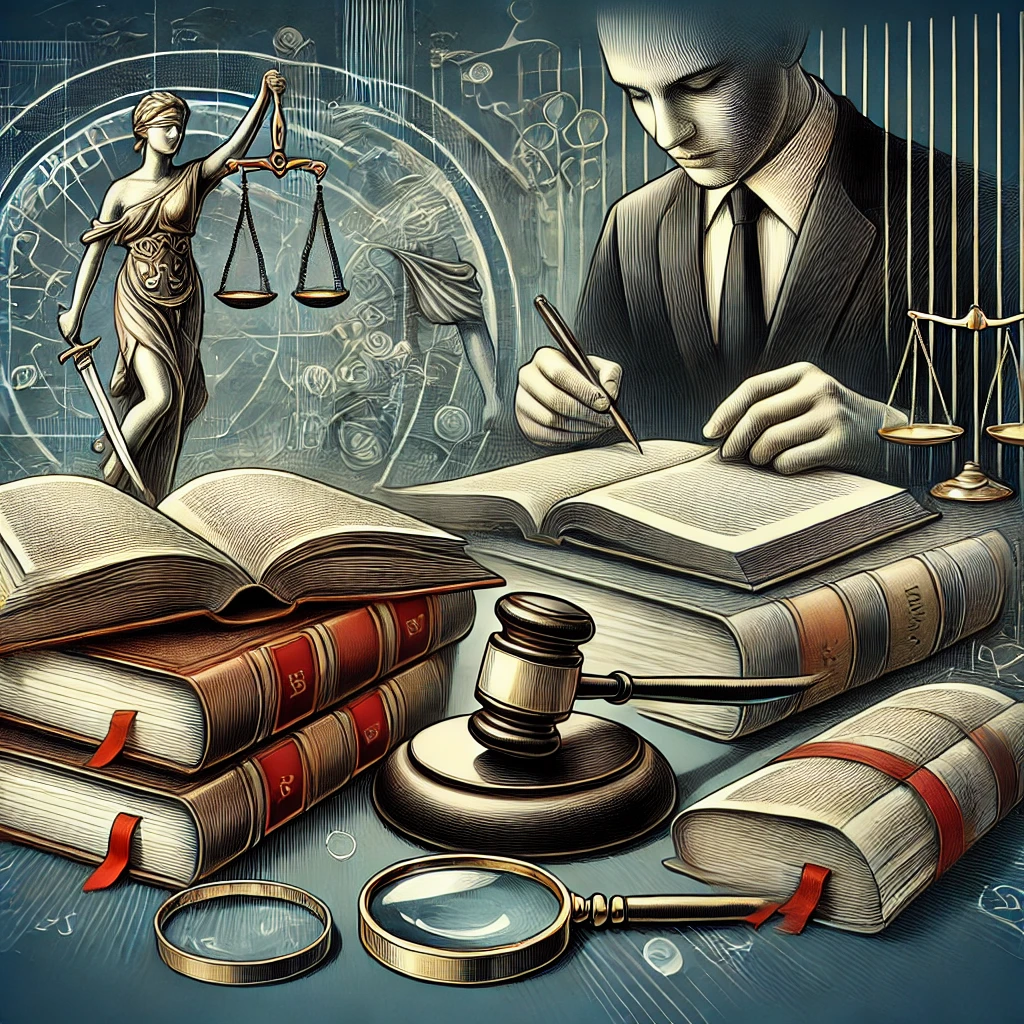प्रश्न 1. अधिवक्ता। Advocates.
उत्तर- अधिवक्ता (Advocate) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (क) के अनुसार, ” अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। यदि कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि के लिए आवश्यक शर्तों को पूर्ण करता है तो उसको अधिवक्ता के रूप में राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित किया जा सकता है। धारा 17 बतलाती है कि प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ताओं को ऐसी नामावली तैयार करेगी एवं रखेगी। अधिवक्ता न्यायालय का आफिसर होता है और उसका यह कर्त्तव्य होता है कि वह न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण रुख या दृष्टिकोण बनाये रखे।
प्रश्न 2. मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त।
Principle of Basic Structure.
उत्तर – केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (AIR 1973 S.C). के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। मूलभूत ढाँचे के सिद्धान्त से अभिप्राय यह है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं निरसन कर सकता है किन्तु संसद संविधान के मूलभूत ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है अर्थात् संसद की संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, उस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त के संदर्भ में केशवानन्द भारती के बाद में उल्लेख किया, किन्तु मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त क्या है, इसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि को संविधान का आधारभूत ढाँचा माना है।
प्रश्न 3. अधिवक्ता के पंजीकरण के लिए अर्हतायें। Qualifications for enrolement as an Advocate.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-24 में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने की ईप्सा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक एक समान शर्तों एवं अर्हताओं का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य की सूची में किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो-
(1) वह भारत का नागरिक हो।
(2) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
(3) उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तीन वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् विधि में स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो, बशर्ते कि इस प्रकार की उपाधि को बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता दी गयी हो।
(4) उसने सम्बन्धित राज्य की बार कौंसिल को देय नामांकन शुल्क की अदायगी कर दी है।
(5) उसे ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है जो राज्य बार कौंसिल द्वारा निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
प्रश्न 4. वाक् की स्वतंत्रता एवं न्यायालय की अवमानना।
Freedom of Speech and Contempt of Court.
उत्तर- वाक् की स्वतंत्रता (Freedom of Speech)- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (क) में बाकू एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। बाकू की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदत्त एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके माध्यम से उनका स्वांगीण विकास होता है, तर्क करने, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के बाक् की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दे तो उस राष्ट्र का शीघ्र ही पतन हो जायेगा क्योंकि राष्ट्र का विकास नागरिकों के स्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है। वाक् की स्वतंत्रता अपने आप में आत्यंतिक नहीं है, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा न्यायालय के अवमान से जुड़ा इन रि अरुंधती राय का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि न्यायालय की गरिमा को बनाये रखना विधि के नियम का एक मूलभूत सिद्धान्त है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की आड़ में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय/न्यायपालिका की गरिमा को कम करने अथवा समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति इस स्वतन्त्रता की आड़ में न्यायपालिका की गरिमा पर प्रहार करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही किया जाना ही एक मात्र उपाय रह जाता है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन की अग्रणी अरुंधती राय द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की न केवल आलोचना की गई थी अपितु न्यायाधीशों पर कई अनर्गल आरोप भी लगाये गये थे। इसे न्यायालय ने अवमान मानते हुए उन्हें एक दिन के कारावास एवं 2,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
प्रश्न 5. एक राज्य सूची से दूसरे राज्य सूची में अधिवक्ता पंजीकरण के स्थानान्तरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
Discuss the procedure of transfer of name of Advocate from one State roll to another State.
उत्तर– एक राज्य सूची से दूसरे राज्य सूची में अधिवक्ता पंजीकरण के स्थानान्तरण की प्रक्रिया के बारे में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-18 में बताया गया है। धारा-18 के अनुसार-धारा-17 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, अपना नाम उस राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अन्तरित कराने के लिए विहित प्ररूप में भारतीय विधिज्ञ परिषद् को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् यह निदेश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम, किसी फीस के संदाय के बिना प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से हटाकर उस अन्य राज्य विभिन परिषद् को नामावली में दर्ज किया जाए और सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगी।
परन्तु जहाँ आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है या जहाँ किसी अन्य कारण से भारतीय विधिज्ञ परिषद् को यह प्रतीत होता है कि अन्तरण के लिए आवेदन सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है और अन्तरण नहीं किया जाना चाहिए वहाँ भारतीय विधिज्ञ परिषद् आवेदन करने वाले व्यक्ति को इस निमित्त अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगी।
प्रश्न 6. राज्य विधिज्ञ परिषदों के कृत्य
Functions of State Bar Councils.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-6 के अधीन राज्य बार कौंसिल को कतिपय कार्य करने होते हैं। बार कौंसिल के कार्य निम्नवत् होंगे –
(क) अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों की प्रविष्टि करना,
(ख) ऐसी नामावली तैयार करना और बनाये रखना,
(ग) अपनी नामावली को अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवचार के मामले ग्रहण करना और उनका अवधारण करना,
(घ) अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों को रक्षा करना,
(ङ) विधि सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना,
(डङ) विधिक विषयों पर प्रतिष्ठित विधिशास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधिक रुचि की पत्र-पत्रिकायें और लेख प्रकाशित करना,
(ङ) विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना,
(च) बार कौंसिल की विधियों का प्रबन्ध और उनका विविधान करना,
(छ) अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना,
(ज) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बार कौंसिल को प्रदत्त सभी कृत्यों का पालन करना।
प्रश्न 7. अधिवक्ता का पारिश्रमिक।
Advocate’s Fee.
उत्तर– भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने अधिवक्ता की फीस के निर्धारण के निमित्त नियम नहीं बनाया है और इस कारण इसका निर्धारण व्यक्तिगत अनुबन्ध द्वारा होता है। इस प्रकार अधिवक्ता और मुवक्किल के मध्य हुए करार द्वारा अधिवक्ता द्वारा की जाने वालो व्यावसायिक सेवा के फीस का निर्धारण होता है। इस बिन्दु पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियम-11 और नियम 38 का उल्लेख करना सुसंगत होगा। नियम-11 के अनुसार अधिवक्ता अपने अवस्थिति और वाद की प्रकृति के अनुसार फीस लेकर मुवक्किल कापसार (ब्रीफ) उस दशा में स्वीकार करने के लिए बाध्य है जबकि वह पक्षसार ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो उस न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में है जिसमें प्रैक्टिस करने का यह प्रस्ताव करता है।
इस प्रकार यह नियम इस बात की ओर इंगित करता है कि फीस का निर्धारण अधिवक्ता की बार में अवस्थिति और बाद की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए।
प्रश्न 8 नामांकन समिति। Enrolment Committee.
उत्तर – प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद की अपनी एक नामांकन समिति होती है जिसका कार्य है यदि किसी व्यक्ति ने विधि स्नातक की उपाधि धारण कर लिया है तो वह सम्बन्धित राज्य विधिज्ञ परिषद् में आवेदन करता है अधिवक्ता के लिए, जिसे राज्य विधिज्ञ परिषद् नामांकन समिति को निर्दिष्ट कर देती है और ऐसी समिति राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए मामले का निपटारा करती है।
परन्तु यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद् का, या तो इस निमित्त उसे किए गये निर्देश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी आवश्यक तथ्य के सम्बन्ध में दुर्व्यपदेशन द्वारा, कपट द्वारा या असम्यक् असर डालकर, अधिवक्ता नामावली में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो वह उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका नाम अधिवक्ता नामावली से हटा सकेगी।
जहाँ किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामांकन समिति, किसी ऐसे आवेदन को इंकार करने का प्रस्ताव करती है वहाँ वह आवेदन को भारतीय विधिज्ञ परिषद् की राय के लिए निर्दिष्ट करेगी और प्रत्येक ऐसे निर्देश के साथ आवेदन से इंकार किए जाने वाले आधारों के समर्थन में विवरण होगा।
प्रश्न 9. अधिवक्ता के समाज के प्रति कर्त्तव्य ।
Duties of an Advocate towards society.
उत्तर- अधिवक्ता, समाज का सच्चे अर्थों में वास्तविक सेवक होता है। अधिवक्ता ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय से उपचार दिलवाने में लोगों की मदद करता है। इसके अलावा अधिवक्ता समाज के दलित, निर्धन एवं असहाय लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करता है। अतः अधिवक्ता का समाज के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है क्योंकि वह समाज में रह रहे व्यक्तियों को न्याय दिलाने में मदद करता है।
प्रश्न 10. पूर्व सुनवाई का अधिकार।
Right of Pre-audience.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-23 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को सम्पूर्ण भारत में सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार है। इस अधिनियम में अवरोही क्रम में पूर्व सुनवाई के उत्क्रमात्मक अधिकार का प्रावधान किया गया है। धारा 23 (1) के अनुसार भारत के महान्यायवादी की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी जिसमें सालिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया भी शामिल है। धारा-23 (2) के अनुसार भारत के महान्यायवादी को छोड़कर अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व भारत के सालिसिटर जनरल की सुनवाई होगी।
इसी प्रकार से अधिनियम की धारा-23 (5) के अंतर्गत यह विधान किया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में परस्पर और अन्य अधिवक्ताओं में परस्पर पूर्व सुनवाई का अधिकार उनकी अपनी-अपनी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित किया जायेगा।
प्रश्न 11. अधिवक्ता एवं मुवक्किल के सम्बन्ध
The relationship of Advocate and client.
उत्तर – एक अधिवक्ता एवं उसके मुवक्किल के बीच का सम्बन्ध निश्चित रूप से वैश्वासिक सम्बन्ध होता है क्योंकि एक अधिवक्ता एवं उसके मुवक्किल के बीच विश्वास का होना अति आवश्यक है। सामान्यतया जहाँ पक्षकारों के बीच वैश्वासिक सम्बन्ध विद्यमान होता है। वहाँ संविदा जैसे कतिपय करार की उपधारणा की जा सकती है।
पी० सी० रामगड़ी राय बनाम डी० गोपालन (AIR 1979 S.C. 281) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि अधिवक्ता एवं उसके मुवक्किल के बीच का सम्बन्ध विशुद्ध रूप से वैयक्तिक होता है जिसमें उच्च श्रेणी का व्यक्तिगत विश्वास अंतर्ग्रस्त रहता है।
प्रश्न 12 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का उद्देश्य।
Object of Advocate Act, 1961.
उत्तर – भारतीय संसद ने सन् 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया, इस अधिनियम का उद्देश्य विधि-व्यवसाय सम्बन्धी विषयों को संकलित और संशोधित करना और राज्य बार कौंसिल तथा अखिल भारतीय बार कौंसिल के गठन के सम्बन्ध में उपबन्ध करना है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 राज्य विधिज्ञ परिषद (State Bar Council) और भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Indian Bar Council) के गठन कार्य और शक्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के मानक का निर्धारण करती है और इसके उल्लंघन पर दण्ड के सम्बन्ध में भी नियम बना सकती है। यह विधि शिक्षा का स्तर निर्धारित करती है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है. जिनकी विधि-स्नातक की डिग्री प्राप्तकर्ता को अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह राज्य विधिज्ञ परिषद् पर नियन्त्रण भी रखती है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती है। अनुशासन कमेटी द्वारा जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उसका निर्धारण भी यही करती है।
प्रश्न 13. अधिवक्ता की पोशाक। Dress of Advocate.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1) (छछ) एवं नियमावली में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों अथवा प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के लिए गणवेश (वर्दी या पोशाक) का प्रावधान किया गया है।
(क) पुरुष अधिवक्ता को निम्नलिखित पोशाक पहनना पड़ेगा –
(i) काला बटन बन्द कोट, अचकन, काली शेरवानी एवं सफेद बैंड तथा अधिवक्ता का गाठन; अथवा
(ii) खुले वक्ष की काली कोट, सफेद शर्ट, सफेद कालर, कोमल अथवा कड़ी सफेद बैंड तथा अधिवक्ताओं द्वारा पहना जाने वाला गाठन।
(iii) लम्बा ट्राउजर (सफेद, काला धारीदार अथवा भूरा) अथवा धोती।
(ख) महिला अधिवक्ता को निम्नलिखित पोशाक पहनना पड़ेगा
(i) काला एवं पूरी अथवा आधी आस्तीन का जैकेट अथवा ब्लाउज, सफेद कालर, मृदु अथवा कड़ी सफेद बैंड और अधिवक्ता का गाउन; अथवा
(ii) सफेद ब्लाउज, कालर सहित अथवा बिना कालर का तथा सफेद बैंड एवं काला खुले वक्षस्थल वाला कोट; अथवा
(iii) साड़ी अथवा लम्बा स्कर्ट (काला, सफेद अथवा किसी भी मध्यम रंग का बिना किसी छींट अथवा डिजाइन का) अथवा पंजाबी पोशाक, (चूड़ीदार कुर्ता अथवा सलवार, कुर्ता, दुपट्टा सहित अथवा दुपट्टा रहित) सफेद अथवा काले रंग का ।
बशर्ते कि अधिवक्ता का गाउन पहनना उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सिवाय ऐच्छिक होगा।
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय अथवा सिटी सिविल कोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय में बैंड के बजाय काली टाई पहनी जा सकती है।
प्रश्न 14. व्यावसायिक अवचार।
Professional Misconduct.
उत्तर- व्यावसायिक अवचार (Professional Misconduct)- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। यदि परिषद् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी रहा है तो राज्य विधिज्ञ परिषद् मामले को अपनी अनुशासन समिति को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगी। यह धारा यह भी स्पष्ट कर देती है कि राज्य विधिज्ञ परिषद् अपनी अनुशासन समिति के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही को या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसको किये गये आवेदन पर वापस ले सकती है और यह निदेश दे सकती है कि जाँच उस राज्य विधिज्ञ परिषद् की किसी अन्य अनुशासन समिति द्वारा की जाय। अनुशासन समिति सम्बद्ध अधिवक्ता और महाधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित में से कोई आदेश पारित कर सकती है –
(क) शिकायत खारिज कर सकती है या यदि राज्य विधिज्ञ परिषद् की प्रेरणा पर कार्यवाहियाँ आरम्भ की गई थीं तो वह यह निदेश दे सकती है कि कार्यवाहियाँ फाइल कर दी जायें।
(ख) अधिवक्ता को भर्त्सना का दण्ड (धिग्दण्ड) दे सकती है।
(ग) अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से उतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकती है, जितनी वह ठीक समझे।
(घ) अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नामावली से हटा सकती है।
स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राम सिंह, ए० आई० आर० 1992 एस० सी० 2188 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवचार’ के अर्थ की व्याख्या करते हुए कहा कि ‘अवचार’ के अन्तर्गत नैतिक अधमता या नैतिक भ्रष्टता सम्मिलित हो सकती है। व्यावसायिक अवचार अनुचित अथवा गलत व्यवहार अवैध व्यवहार आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन इत्यादि के रूप में हो सकता है।
‘अवचार’ एक वृहद् अवधारणा है, किसी आचरण को अवचार के रूप में लेने के लिए। यह आवश्यक है कि उसमें नैतिक अधमता संलग्न हो। आचरण उस स्थिति में अवचार हो सकता है जबकि उसमें नैतिक अधमता न हो। कोई भी आचरण जो किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने से अनुपयुक्त बनाता है, वह व्यावसायिक अवचार होता है। यदि अधिवक्ता का आचरण ऐसा होता है जो उसे सम्मानजनक विधिक व्यवसाय का सदस्य बने रहने में उसे अयोग्य बना देता है अथवा जिन कर्त्तव्यों का सम्पादन अधिवक्ता करते हैं उन्हें सौंपे जाने में उसे अनुपयुक्त बना देता है। नवरतनमल चौरसिया बनाम एम० आर० मुर्ली, ए० आई० आर० 2004 एस० सी० डब्ल्यू० 2894 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अवचार, अन्य के साथ अनुशासन भंग को इंगित करता है। यद्यपि कि पूर्णरूप से यह विहित करना सम्भव नहीं है कि कौन-सा आचरण अथवा अनुशासन भंग गठित करेगा।
प्रश्न 15. विधिज्ञ परिषदें। Bar Councils.
उत्तर- अधिवक्ता अधिनियम दो प्रकार के विधिज्ञ परिषदों के गठन का उपबन्ध करता हैं
(1) राज्य विधिज्ञ परिषद् तथा
(2) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ।
राज्य विधिज्ञ परिषद् (State Bar Council) – अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 में राज्य विधिज्ञ परिषद् के गठन के बारे में बताया गया है।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा उसे स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के अर्जन एवं धारण करने की तथा संविदा करने की शक्ति प्राप्त होगी। धारा 6 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद् अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यक्ति को प्रविष्ट करने, नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों के विरूद्ध अवचार मामले ग्रहण करने, नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करने, विधि सुधार का उन्नयन करने, अपने सदस्यों व्यवस्था करने, विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आयोजन करने, विधिज्ञ परिषद् के निधियों का प्रबन्ध एवं उनका विनिधान करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।
भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Indian Bar Council) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 4 (1) के अनुसार उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, भारतीय विभिन्न परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्
(क) भारत का महान्यायवादी, पदेन;
(ख) भारत का महासालिसिटर, पदेन तथा
(ग) प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा, अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य।
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 (1-क) यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास धारा 3 (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ न हो। इसी अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परिषद् का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा जो उस परिषद् द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो विहित की जाए।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 (2-क) यह स्पष्ट करती है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा।
परन्तु ऐसा व्यक्ति अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन तब तक करता रहेगा जब तक कि परिषद् का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पश्चात् निर्वाचित हुआ है, पदभार सम्भाल नहीं लेता।
इस अधिनियम की धारा 4 (3) यह प्रावधान करती है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के ऐसे सदस्य की, जो राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया हो, पदावधि –
(i) राज्य विधिज्ञ परिषद् के ऐसे सदस्य की दशा में, जो वह पद पदेन धारण करता हो, उसके निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष होगी या उस अवधि तक होगी जिसको वह राज्य विधिज्ञ परिषद् का सदस्य न रह जाए, इनमें से जो भी अवधि पहले हो; और
(ii) किसी अन्य दशा में, उतनी अवधि के लिए होगी जितनी के लिए वह राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण करता हो।
प्रश्न 16. अधिवक्ता नामावली में परिवर्तन।
Alteration in roll of Advocates.
उत्तर- राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ताओं की सूची तैयार करती है और इसकी प्रतिलिपि भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजती है। इस सूची में जिन अधिवक्ताओं का नाम होता है, वह भारत के किसी भी न्यायालय में प्रेक्टिस कर सकते हैं। यह अधिवक्ताओं को नामावली होती है। नामावली में परिवर्तन के लिए अधिनियम की धारा 26 (क) के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद् को किसी भी उस अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली से हटाने की शक्ति है जिसकी या तो मृत्यु हो गयी हो या जिससे नाम हटाने का आवेदन पत्र प्राप्त हो गया हो।
जहाँ ऐसा कोई वरिष्ठ अधिवक्ता 31 दिसम्बर, 1965 के पहले उस विधिज्ञ परिषद् को जो ऐसी नामावली रखती है जिसमें उसका नाम दर्ज किया गया है, आवेदन करता है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं बना रहना चाहता है वहाँ, विधिज्ञ परिषद् उस आवेदन को मंजूरी दे सकेगी और तद्नुसार नामावली परिवर्तित की जाएगी।
प्रश्न 17. अधिवक्ता लेखांकन के बारे में बताइए।
Discuss about Advocate Accountancy.
उत्तर- अधिवक्ता लेखांकन (Advocate Accountancy) अधिवक्ता को व्यापार अथवा हानि-लाभ लेखा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अधिवक्ता वृत्तिक कार्य करता है और यह व्यापार नहीं होता है। अधिवक्ता को प्राप्ति और संदाय लेखा, आय व्यय लेखा और बैलेंसशीट बनाना आवश्यक है। प्रत्येक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के नाम में खाता तैयार करना चाहिए और उसमें क्रेडिट (Credit) और डेबिट (Debit) दो कॉलम बनाना चाहिए। मुवक्किल के लिए अथवा उसके द्वारा प्राप्त धनराशि को क्रेडिट में और उसकी ओर से खर्च की गई राशि अथवा प्रदत्त राशि को डेबिट में दर्शाना चाहिए।
अधिवक्ता अपना प्राप्ति और संदाय लेखा अपनी रोकड़ पुस्तिका के आधार पर तैयार करता है।
आय व्यय लेखा में अधिवक्ता पूरे वर्ष की आय और व्यय का उल्लेख करता है। इससे अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है।
इन्हीं के आधार पर अधिवक्ता को अपना बैलेंसशीट भी तैयार करना होता है। अधिवक्ता भी अपना बैलेंसशीट उसी प्रकार तैयार करता है जैसा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता है। बैलेंसशीट से यह जानकारी मिल जाती है कि आय व्यय से अधिक है अथवा व्यय आय से अधिक है। इससे सम्बन्धित इसमें संक्षिप्त कथन होता है।
लेखा-कर्म (Accountancy) के उद्देश्य और लाभ इस प्रकार हैं
(क) जिन स्रोतों से धन प्राप्त हुआ है और जिन प्रयोजन और मदों पर व्यय हुआ उसका ज्ञान होता है और तुरन्त इसकी जानकारी हो जाती है।
(ख) अधिवक्ता को इस बात की जानकारी हो जाती है कि प्राप्ति व्यय से अधिक है अथवा इससे कम
(ग) वर्ष की समाप्ति पर उसे इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि उसके पास नगद राशि कितनी है।
(घ) व्यय की प्रकृति का भी ज्ञान हो जाता है।
(ङ) मुवक्किल की कितनी रकम अधिवक्ता के पास है और कितनी रकम मुवक्किल द्वारा अधिवक्ता को दी जानी है, इसकी जानकारी सुगमता से प्राप्त हो जाती है।
(च) वित्तीय वर्ष में अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है।
(छ) पिछले वर्ष और चालू वर्ष का तुलनात्मक अध्ययन करना भी आसान हो जाता है।
(ज) वित्तीय वर्ष अथवा गतवर्ष के अन्त में आयकर और धन कर विवरणी तैयार करने में भी सुगमता होती है। अधिवक्ताओं को कई प्रकार की छूट उपलब्ध है परन्तु इसके लिए रसीद की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित लेखाकर्म से आयकर और धन विवरणी भरने के साथ ही छूटों का दावा करने में भी सुगमता होती हैं।
(झ) लेखाकर्म का उद्देश्य कारबार अथवा पेशे की सम्पत्ति का अनुचित प्रयोग रोकना और वित्तीय संव्यवहार का सुनियोजित अभिलेख अनुरक्षित करना भी है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य पेशे या कारबार से होने वाले शुद्ध लाभ को विनिश्चित करना भी है।
प्रश्न 18 वरिष्ठता के बारे में विवाद।
Dispute about seniority.
उत्तर- वरिष्ठता के बारे में विवाद- अधिवक्ता अधिनियम की धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि जहाँ दो या उससे अधिक व्यक्तियों की वरिष्ठता की तारीख एक ही हो, वहाँ आयु में वरिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वरिष्ठ माना जायेगा। यदि किसी व्यक्ति की वरिष्ठता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे विनिश्चय हेतु सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा।
प्रश्न 19. वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है?
Who is senior advocate?
उत्तर- वरिष्ठ अधिवक्ता– भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम के भाग-VI का अध्याय-1 वरिष्ठ अधिवक्ता के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। विधि व्यवसाय के मामले में कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता किसी भी ऐसे न्यायालय, प्राधिकरण जिसका उल्लेख अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 में किया गया है, के समक्ष अपना वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा या कोई कार्य नहीं करेगा। कोई कार्य नहीं करने का अर्थ यह है कि किसी ऐसे न्यायालय, या अधिकरण से है, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 30 में किया गया है।
बार को वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता में विभाजित करने का सुझाव सन् 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट में दिया था। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 में अधिवक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है पहला वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरा अन्य अधिवक्ता कोई भी अधिवक्ता अपनी सम्मति से, वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम ले सकेगा, ऐसा तब होगा जब सर्वोच्च न्यायालय की अथवा हाईकोर्ट की यह राय हो कि वह अपनी योग्यता, विधि-व्यवसायी वर्ग में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव के आधार पर ऐसा सम्मान प्राप्त करने के योग्य है।
पश्न 20. विधिक व्यवसाय का महत्व।
Importance of legal profession.
उत्तर- विधिक व्यवसाय का महत्व – विधिक व्यवसाय अत्यन्त सम्मानजनक व्यवसाय है। इसका सृजन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि लोकहित के लिए किया गया है( न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायाधीशों को सही निर्णय देने में अधिवक्ता सहायता प्रदान करते हैं। अधिवक्ता वाद से सम्बन्धित विधिक सामग्री एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इस सामग्री के आधार पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। अधिवक्ताओं के अभाव में न्यायाधीश के लिए सही निर्णय देना एक अलौकिक कार्य होगा।
प्रश्न 21. वृत्तिक आचार। Professional Ethics.
उत्तर- व्यावसायिक आचार (Professional Ethics)- व्यावसायिक आचार से तात्पर्य ऐसे आचरण की संहिता से है जो चाहे लिखित हो या मौखिक परन्तु विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं के स्वयं के प्रति अपने मुवक्किल के प्रति, विधि में अपने प्रतिपक्षी के प्रति और न्यायालय के प्रति उसके व्यवहार को विनियमित करती हो।
वृत्तिक- आचार का मुख्य उद्देश्य विधिक व्यवसाय के सम्मान और मर्यादा को बनाए रखना और अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना है। न्यायमूर्ति मार्शल एवं डॉ० सी० एल० आनन्द ने भी उपरोक्त उद्देश्य का समर्थन किया।
प्रश्न 22. न्यायालय अवमान सम्बन्धी सांविधानिक उपबंध।
Constitutional provisions relating to Contempt of Court.
उत्तर – भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में परिगणित विषयों में से किसी भी नियम के विषय में संसद को विधि निर्माण की अनन्य शक्ति प्रदान की गयी है। सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधान मंडल दोनों उसमें गिनाये गये किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। फिर भी संसद एवं राज्य विधान मंडल की विधियों के मध्य संघर्ष होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होती है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 अर्थात् संघ सूची की प्रविष्टि 77 में तथा सूची-III अर्थात् समवर्ती सूची की प्रविष्टि-14 में न्यायालय की अवमानना का विषय शामिल है। संविधान के इस प्रावधान को दृष्टिपथ में रखते हुए सान्याल कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि व्यवस्थापिका को न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में विधि निर्माण करने की सांविधानिक प्राधिकार प्राप्त है किन्तु व्यवस्थापिका को अवमानना हेतु दण्डित करने की सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती करने अथवा इस शक्ति के किसी अन्य न्यायालय में निहित करने की शक्ति नहीं प्राप्त है।
संविधान के अनुच्छेद 142 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा निर्मित किसी शक्ति के अधीन अपनी अवमानना करने वाले को दण्डित करने हेतु कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है और इस प्रकार से संसद को उच्चतम न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान गयी है।
प्रश्न 23. भारतीय विधिज्ञ परिषद् की शक्तियाँ।
Powers of Indian Bar Council.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-15 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् को नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नियम बनाने की शक्ति में निम्नलिखित नियम आते हैं –
(i) भारतीय बार कौंसिल के सदस्यों का ग्रुप मतदान द्वारा निर्वाचन, जिसके अन्तर्गत वे शर्ते भी हैं जिसके अधीन रहते हुए व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
(ii) विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति।
(iii) विधिज्ञ परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों का भरना।
(iv) विधिज्ञ परिषद् के अधिवेशन बुलाना और उनका आयोजन उनके कारबार का संचालन और उनमें गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या।
(v) विधिज्ञ परिषद् द्वारा लेखा-बहियों तथा अन्य पुस्तकों का रखा जाना।
(vi) अधिवक्ता के रूप में प्रविष्टि [ धारा-20]
(vii) अनुशासन समितियों तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति
(viii) वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए दण्ड देने की शक्ति
(ix) अपीलीय शक्ति।
प्रश्न 24. न्यायालय की अवमानना।
Contempt of Court.
उत्तर- न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा-2 (क) के अनुसार ‘न्यायालय की अवमानना’ का तात्पर्य होता है सिविल अवमानना अथवा दाण्डिक अवमानना। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय की अवमानना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गयी है किन्तु अवचार के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें न्यायालय की अवमानना के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए :
(क) न्यायालय के विरुद्ध अपमानास्पद भाषा का प्रयोग करने तथा न्यायाधीश के विरुद्ध अपमानास्पद अभिकथनों का किया जाना।
(ख) न्यायाधीश के विरुद्ध कलंकित अभिकथन करना।
(ग) मनमाफिक आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों को दबाना।
(घ) न्यायाधीश को दिखा कर जूता लहराना,
(ङ) पक्षपात का अभियोग लगाना,
(च) न्यायाधीश के विरुद्ध अनुचित कार्य किया जाना,
(छ) किसी अधिवक्ता अथवा उसके मुवक्किल द्वारा न्यायालय के आदेश की भी अवज्ञा करना,
(ज) न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर उक्त अधिवक्ता द्वारा न दिया जाना।
प्रश्न 25. आपराधिक अवमान। Criminal Contempt.
उत्तर– न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा-2 (ग) में आपराधिक अवमान की परिभाषा दी गयी है। इसके अनुसार आपराधिक अवमान से तात्पर्य किसी बात के प्रकाशन (चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो अथवा चिन्ह हो या वह दृश्यरूपेण हो अथवा किसी अन्य तरीके से हो) अथवा किसी अन्य कार्य से है, जो कि :
(i) किसी न्यायालय को कलंकित करने अथवा उसके प्राधिकार या सत्ता को न्यून करता है अथवा करने की प्रवृत्ति रखता हो।
(ii) किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक् अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या उसमें अड़चन पैदा करता हो या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता हो, अथवा
(iii) किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में अड़चन पैदा करता है या अड़चन पैदा करने की प्रवृत्ति रखता हो।
इस प्रकार से यदि किसी कृत्य अथवा कार्यवाही में इनमें से उपस्थित तत्वों में से कोई भी तत्व पाया जाता है तो उसे अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय की दाण्डिक अवमानना माना जायेगा।
टी० एन० दीन दयाल बनाम हाईकोर्ट (AIR 1997 S.C.) के मामले में न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया था कि जहाँ अवमानकर्ता ने उच्च न्यायालय के विरुद्ध निराधार अभिकथन करके निर्वाचन याचिका के अंतरण हेतु आवेदन दाखिल किया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ये अभिकथन अवमानना कारक थे और इनका आशय न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा-2 (म) के अधीन न्यायालय को कलंकित करना था।
प्रश्न 26 बार-बेंच सम्बन्ध । Bar-Bench relation.
उत्तर– न्याय के प्रशासन में बेंच एवं बार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेंच विधि का प्रशासन बार की सहायता से करती है। न्यायालय द्वारा बहुत से अवसरों पर यह घोषणा न्यायिक रूप से की गयी है कि अधिवक्तागण अर्थात् बार के सदस्य न्यायालय के अधिकारी होते हैं। बार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मामले के सुसंगत सामग्री को एकत्र करें और उसके द्वारा सही निर्णय पर पहुँचने में न्यायालय की सहायता करे।
हनीराज एल० चुलानी बनाम बार कौंसिल ऑफ महाराष्ट्र एण्ड गोवा (AIR 1996 S.C. 1708) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया था कि विधि व्यवसाय अर्थात् बार न्यायपालिका की भागीदार होती है और न्याय के प्रशासन में ‘बार’ को अपना सर्वोत्तम योगदान करना चाहिए। चूँकि न्यायालय अपना कार्य अधिवक्ताओं के कथन के आधार पर करती है इसलिए अधिवक्ताओं का यह कर्त्तव्य है कि वे न्यायालय का सम्मान करें और अपनी स्वच्छ छवि बनाये रखें। अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे न्यायालय के समक्ष सही कथन करें और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत न करें।
पी० डी० गुप्ता बनाम राममूर्ति (AIR 1998 S.C. 283) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्याय का प्रशासन एक सरिता है, जिसे हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ रखने की जरूरत है। इसे हमेशा प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। न्याय के प्रशासन का सम्बन्ध केवल बेंच से नहीं है, इसका सम्बन्ध बार से भी है।
प्रश्न 27. अधिवक्ता का मुवक्किल के प्रति कर्त्तव्य ।
Duties of an Advocate towards client.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1) (ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् को शक्ति प्रदान करती है कि वह अधिवक्ताओं द्वारा पालन किये जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक को विहित कर सके। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों जो कि अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्त्तव्यों को दर्शाता है कुछ निम्न हैं :
(1) अधिवक्ता अपनी अवस्थिति और वाद की प्रकृति के अनुसार फीस लेकर मुवक्किल का पक्षसार (बीफ) उस स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य है जबकि वह पक्षकार ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो उस न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में है जिससे प्रैक्टिस करने वह प्रस्ताव करता है।
(2) यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है तो सामान्यत: बिना पर्याप्त कारण के और मुवक्किल को बिना युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना दिए पैरवी करने से इन्कार नहीं कर सकता।
(3) प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भय होकर उचित और सम्मानजनक तरीके से करे।
(4) अधिवक्ता मुकदमेबाजी उकसाने में किसी भी समय पक्षकार नहीं बनेगा।
(5) कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के निदेशों पर कार्य नहीं करेगा।
प्रश्न 28 राज्य विधिज्ञ परिषद् । State Bar Council.
उत्तर- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3′ में प्रावधान किया गया है कि राज्य विधिज्ञ परिषदों की स्थापना की जायेगी।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा उसे स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के अर्जन एवं धारण करने की तथा संविदा करने की शक्ति प्राप्त होगी। धारा 6 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद् अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में व्यक्ति को प्रविष्ट करने, नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों के विरूद्ध अवचार मामले ग्रहण करने, नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करने, विधि सुधार का उन्नयन करने, अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करने, विहित रीति से निर्धनों को विहित सहायता प्रदान करने के लिए आयोजन करने, विधिज्ञ परिषद् के निधियों का प्रबन्ध एवं उनका विनिधान करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।
प्रश्न 29. वृत्तिक कदाचार के लिए दण्ड।
Punishment for professional misconduct.
उत्तर– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दण्ड का उपबन्ध करती है। इसके अनुसार यदि किसी शिकायत की प्राप्ति पर अथवा अन्य किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक (व्यावसायिक) या अन्य अवचार का दोषी रहा है तो वह मामले को अनुशासन समिति को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगी। वह इसकी जाँच का आदेश कर सकती है।
अनुशासन समिति अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित में से कोई आदेश पारित कर सकती है
(क) शिकायत खारिज कर सकती है या सम्बन्धित राज्य विधिज्ञ परिषद् को कार्यवाहियों को फाइल करने का निर्देश दे सकती है।
(ख) अधिवक्ता को भर्त्सना का दण्ड
(ग) राज्य नामावली में से अधिवक्ता के नाम को हटा सकती है।
(घ) अधिवक्ता को विधि व्यवसाय के लिए उतनी अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकती है, जितना वह उचित समझे।
प्रश्न 30. अधिवक्ताओं द्वारा अवमानना
Contempt by Advocates.
उत्तर- अधिवक्ताओं द्वारा अवमानना- अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति के कारण वे अक्सर उत्तेजनापूर्ण वाद-विवाद करने लग जाते हैं जिसका परिणाम न्यायालय की अवमानना के रूप में हो सकता है। कदाचार के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें न्यायालय के अवमान के रूप में ग्रहण किया गया है अर्थात् किसी न्यायाधीश के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, न्यायाधीश के प्रति कलंकपूर्ण अभिकथन करते हुए अपमानास्पद शब्दावली का प्रयोग करना, किसी न्यायाधीश के प्रति कलंकपूर्ण अभिवाक् करना, अनुकूल आदेश पारित कराने के लिए तथ्यों को दबाना, न्यायाधीश को जूता दिखाना, न्यायाधीश के विरुद्ध पक्षपात एवं अनुचित कार्य के सम्बन्ध में झूठा कथन करना आदि। यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्यायालय की अवज्ञा करने की सलाह देता है तो उसे भी न्यायालय की अवमानना का दायी माना जायेगा। किसी बार कौंसिल के निर्वाचन के दौरान न्यायपालिका पर प्रहार करना भी न्यायालय की अवमानना माना जाता है। यदि कोई अधिवक्ता न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर देता है तो उसे भी न्यायालय की अवमानना का दायी ठहराया जायेगा। इन री अजय कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 3299 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी अधिवक्ता द्वारा अनियन्त्रित भाषा का प्रयोग करना और विभिन्न न्यायिक अधिकारियों पर झूठा आरोप लगाना और न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय उन पर हेतु को मान्यता देने आदि को न्यायालय की घोर अवमानना माना जायेगा। इस मामले में अधिवक्ता को चार महीने के साधारण कारावास का तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया गया था।
कोई भी अधिवक्ता अभिवचन अथवा बहस के दौरान किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है जो असंसदीय होगी और जिसकी प्रवृत्ति न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने अथवा न्यायालय की प्रतिष्ठा एवं विधि के आदर्श को गिराने की होगी।
इनरी विनय चन्द्र मिश्र, ए० आई० आर० 1995 एस० सी० 2348 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा पूछे गये प्रश्न से नाराज हो जाना, उनके प्रति असम्मानजनक रवैया अपनाना, प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में उसके प्राधिकार पर प्रश्न चिह्न लगाना, उसके ऊपर चिल्लाना तथा उसे स्थानान्तरण एवं महाभियोग के लिए धमकाना तथा पारित किये जाने योग्य आदेश लिखवाने के लिए उसके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना तथा उसे अपशब्द कहना, न्यायालय में इस प्रकार के दृश्य का सृजन करना और न्यायाधीश से मस्तिष्क का संतुलन खोकर बातचीत करना जैसे कार्य ऐसे कृत्य हैं जो न्याय के अनुक्रम में हस्तक्षेप एवं बाधा माने जाते हैं।
प्रश्न 31. न्यायाधीशों द्वारा अवमानना। Contempt by Judges.
उत्तर- न्यायाधीशों द्वारा अवमानना (Contempt by Judges) – न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 16 (1) के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसी प्रकार दायी माना जायेगा जिस प्रकार से कोई अन्य व्यक्ति दायी होता है और इस अधिनियम के प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे।
इसके आगे धारा 16 (2) में यह कहा गया है कि इस धारा में की कोई बात किसी अधीनस्थ न्यायालय के सम्बन्ध में किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष उस अधीनस्थ न्यायालय के आदेश या निर्णय के विरुद्ध लम्बित किसी अपील अथवा पुनरीक्षण में ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये किसी सम्प्रेक्षण या की गयी किसी टिप्पणी (remark) पर लागू नहीं होगी।
यदि कोई न्यायाधीश अपशब्दों का प्रयोग करता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो फूहड़ प्रतीत होती है, तो न्यायपीठ की यश और प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का लगता है और उक्त न्यायाधीश को न्यायालय की अवमानना करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरणार्थ मोहम्मद शफी एडवोकेट बनाम चौधरी कादिर बक्श (ए० आई० आर० 1949 लाहौर 270) के मामले में सुनवाई की तिथि को अधिवक्ता ने यह अभिवाक् किया था कि उसके मुवक्किल ने याची के विरुद्ध उप न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही से लेकर वाद के निस्तारण तक के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात् मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया था और अधिवक्ता से कहा था,,,,,,,
यह एक मूर्ख अधिवक्ता द्वारा संस्थित बाद में एक मूर्ख उप-न्यायाधीश द्वारा पारित मूर्खतापूर्ण आदेश है। तुम कहाँ से आये हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? ऐसा लगता है कि तुम्हें कानून को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। तुम मूर्खतापूर्ण आदेश के उपाप्त करने (procure) के उपकरण हो और इस तरह से तुमने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें जेल के सलाखों के भीतर भेजा जा सकता है।
मजिस्ट्रेट की इस प्रकार की टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना माना गया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट ने न केवल उप-न्यायाधीश (Sub-Judge) के प्रति न्यायालय की अवमानना की थी बल्कि उसने अधिवक्ता के प्रति भी अवमानना की थी, जो न्यायालय का एक अधिकारी होता है।
प्रश्न 32. भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अपीलीय शक्तियाँ Appellate powers of the Bar Council of India.
उत्तर – भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अपीलीय शक्तियाँ (Appeallate powers of the Bar Council of India)- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 37 भारतीय विधिज्ञ परिषद् को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इस अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत दिये गये राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति के आदेशों के विरुद्ध की गई अपील को सुन सकती है। इसके अनुसार किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति की धारा-35 के अधीन दिये गये आदेश या राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित व्यक्ति, आदेश की संसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अपील कर सकेगा। प्रत्येक ऐसी अपील की सुनवाई भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी और वह समिति उस पर ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड को परिवर्तित कराने का आदेश भी है, पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे। परन्तु भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति का कोई भी आदेश, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जायेगा जिससे कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2003, ए० आई० आर० एस० सी० डब्ल्यू0 43 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अधिवक्ता पर अनुशासनात्मक अधिकारिता यद्यपि कि विधिज्ञ परिषदों में निहित है परन्तु धारा 38 के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में अन्तिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय है।
प्रश्न 33. अनुशासन समिति की शक्तियाँ। Powers of disciplinary committee.
उत्तर- अनुशासन समिति की शक्तियाँ (Powers of disciplinary committee)- अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 राज्य विधिज्ञ परिषद् को तथा धारा 36 भारतीय विधिज्ञ परिषद् को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह कतिपय परिस्थितियों में, मामले को निपटारे के लिए अपनी अनुशासन समिति को निर्दिष्ट कर सकती है। अनुशासन समिति उन मामलों की जाँच करेगी जो राज्य या भारतीय विधिद्ध परिषद् द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किये जायेंगे। अनुशासन समिति को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में विहित है, अर्थात्-
(क) किसी व्यक्ति का समन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
(ख) किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट करने तथा पेश करने की अपेक्षा करना;
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना; तथा
(भं) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।
(ङ) कोई अन्य बात जो विहित की जाए।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 (3) राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति, सम्बद्ध अधिवक्ता और महाधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आदेशों में से कोई आदेश कर सकेगी, अर्थात्-
(क) शिकायत खारिज कर सकेगी।
(ख) अधिवक्ता को धिग्दण्ड दे सकेगी।
(ग) अधिवक्ता को विधि-व्यवसाय से उतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे।
(घ) नामावली से अधिवक्ता का नाम हटा सकेगी।
प्रश्न 34 विधिक सहायता समिति । Legal Aid Committee.
उत्तर—विधिक सहायता समिति (Legal Aid Committee) – अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 (क) के अन्तर्गत विधिज्ञ परिषद् एक या अधिक सहायता विधिक समितियों का गठन करेगी। इस समिति में अधिक से अधिक नौ तथा कम से कम पाँच ऐसे सदस्य होंगे जो विहित किये जायें। विधिक सहायता समिति के सदस्यों की अहंताएँ, उनके चयन की पद्धति तथा उनकी पदावधि वह होगी जो विहित की जाये।
प्रश्न 35. अनुशासन समिति । Disciplinary Committee.
उत्तर- अनुशासन समिति (Disciplinary Committee)—अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 के अनुसार बार कौंसिल एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक ऐसी समिति तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। इसमें दो परिषदों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और तीसरा परिषद् ऐसे अधिवक्ताओं में से सहयोजित व्यक्ति होगा जिसके पास धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अर्हतायें हों और जो परिषद् • का सदस्य न हो। किसी अनुशासन समिति के सदस्यों में से ज्येष्ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक बार कौंसिल एक सचिव नियुक्ति कर सकेगी और एक लेखपाल और ऐसे अन्य व्यक्तियों को अपने कर्मचारी वृन्द के रूप में नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझेगी। धारा 11 की उपधारा (2) के अनुसार सचिव एवं लेखपालों की यदि कोई होंगे, तो वही अर्हतायें होंगी जो विहित की जायेगी।
प्रश्न 36. विधिक शिक्षा समिति। Legal Education Committee.
उत्तर – विधिक शिक्षा समिति (Legal Education Committee) — भारतीय विधिज्ञ परिषद् या धारा 7 (ज) में विधि शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों से विचार-विमर्श करने सम्बन्धी कृत्य समिति के जरिये किया जाता है।
प्रश्न 37. सिविल अवमानना । Civil Contempt.
उत्तर- सिविल अवमान (Civil Contempt) — सिविल अवमान की प्रक्रिया में ऐसे कार्य अथवा लोप (चूक) के रूप में लिया जाता है जिसमें न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा अन्य प्रक्रिया की अवहेलना द्वारा व्यक्तिगत क्षति अन्तर्ग्रस्त होती है। इस प्रकार सिविल अवमान में न्यायालय के आदेश अथवा न्यायालय को दिये गये परिवचन का अपालन किया जाता है और इससे निजी पक्षकार को क्षति होती है और इस कारण निजी पक्षकार का इसके लिए दण्ड देने की कार्यवाही में विशेष रुचि होती है।
इस प्रकार सिविल अवमान उस न्यायिक आदेश के पालन में चूक को कहते हैं जो आदेश प्रतिपक्षी पक्षकार के लाभ के लिए पारित होता है।
विद्यासागर बनाम तृतीय एडिशनल जिला जज, 1991 क्रि० लां० ज० 2286 इला० के मामले में न्यायालय ने कहा कि सिविल अवमान के लिए कार्यवाही का प्रयोजन केवल ‘अवमान के लिए दण्ड देना ही नहीं होता है बल्कि न्यायालय के आदेश का पालन करना और कार्यान्वित करना भी होता है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश को शीघ्र और तत्काल कार्यान्वित कराने का यह एक तरीका है। इसके द्वारा आदेश का शीघ्र और तत्काल पालन कराया जा सकता है।
आवश्यक तत्व- सिविल अवमान के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
(1) न्यायालय के आदेश, डिक्री इत्यादि का अपालन हुआ अथवा न्यायालय को दिये गये परिवचन का भंग या उल्लंघन हुआ है।
(2) यह अपालन या उल्लंघन जानबूझकर किया गया है।
प्रश्न 38 सिविल अवमान में प्रतिरक्षाओं का वर्णन कीजिए। Discuss the defences in civil contempt.
उत्तर- सिविल अवमान की कार्यवाही में प्रतिरक्षायें – सिविल अवमान की कार्यवाही में कब व्यक्ति दण्ड के लिए दायी नहीं होगा, की प्रतिरक्षायें निम्न हैं-
(1) अवज्ञा अथवा भंग जानबूझकर नहीं किया गया था – सिविल अवमान हेतु न्यायालय के आदेश, डिक्री आदि की अवज्ञा अथवा न्यायालय को दिये गये वचन का भंग जानबूझकर किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, अवमान की कार्यवाहियों में यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा होगी कि अवज्ञा अथवा भंग जानबूझकर नहीं किया गया था।
(2) आदेश अधिकारिता के बिना ही पारित कर दिया गया है– यदि अवज्ञा किया गया आदेश न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बिना ही पारित किया गया साबित हो जाता है अथवा उल्लंघन किया गया वचन ऐसी कार्यवाही में दिया गया साबित होता है जो अधिकारिता से रहित थी तो अवज्ञा अथवा उल्लंघन को न्यायालय का अवमान नहीं माना जाता है। वस्तुतः अधिकारिता से रहित पारित आदेश शून्य होता है और शून्य आदेश किसी को भी बाधित नहीं करता है।
(3) जहाँ अवज्ञा किया गया आदेश अस्पष्ट अथवा संदिग्धार्थ हो– अवमान की कार्यवाही में यह कहना प्रतिरक्षा होगी कि आदेश अस्पष्ट अथवा संदिग्धार्थ था। किसी आदेश को अस्पष्ट केवल तब कहा जाता है जब यह विनिर्दिष्ट एवं पूर्ण नहीं होता है। न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के लिए अवमान कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने हेतु आदेश का विनिर्दिष्ट एवं पूर्ण होना आवश्यक होता है।
(4) आदेश में एक से अधिक युक्तियुक्त व्याख्यायें अन्तर्ग्रस्त होती हैं (Order involves more than one reasonable interpretation) – यदि न्यायालय के आदेश में एक से अधिक युक्तियुक्त एवं यथार्थ व्याख्यायें अन्तर्ग्रस्त होती हैं और प्रत्यर्थी उनमें से एक को अंगीकार कर लेता है और उसी व्याख्या के अनुसार कार्यवाही करता है तो उसे न्यायालय के अवमान के लिए दायी नहीं ठहराया जायेगा। परन्तु यदि कोई सन्देह न हो और सन्देह उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है तो इस प्रतिरक्षा की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
(5) आदेश का अनुपालन असम्भव होने पर।
प्रश्न 39. न्यायालय अवमान के लिए दण्ड। Punishment for Contempt of Court.
उत्तर- न्यायालय अवमान अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये दण्ड- न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 12 (1) में यह उपबन्धित है कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में अथवा किसी अन्य कानून में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर के न्यायालय अवमान के लिए साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। किन्तु न्यायालय का समाधान होने पर क्षमादान पर अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है।
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12 (2) में यह कहा गया है कि तत्समय प्रवृत्त कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय किसी अवमान के लिए चाहे वह स्वयं उसकी ही हो या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय की हो या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अवचार हो, इस दण्डादेश से जो धारा 12 (1) में विनिर्दिष्ट है, अधिक अधिरोपित नहीं करेगा। बार कौंसिल की इस विधिक ताकत को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छीना जा सकता है। कोई अवचार न्यायालय के अवमान के साथ ही साथ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ के अन्तर्गत व्यावसायिक या अन्य अवचार भी समझा जायेगा। इस तरह की दशा में, न्यायालय अधिवक्ता को न्यायालय के अवमान के लिए दण्ड दे सकता है तथा ऐसे मामले को बार कौंसिल के पास उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज सकता है, जिससे कि उसको अवचार के लिए दण्ड दिया जा सके। बार कौंसिल अधिवक्ता के अनुज्ञप्ति-पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकती है। अगर बार कौंसिल अधिवक्ता को दण्ड देने के लिए उपयुक्त कार्यवाही नहीं करती है, तब सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 38 के अन्तर्गत अपनी अपीलीय अधिकारिता के इस्तेमाल में बार कौंसिल की कार्यवाहियों को भेज सकता है तथा उसके लिए उचित आज्ञा कर सकता है।
वी० सी० मिश्र, AIR 1995 SC 2348 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अवमान की अधिकारिता के इस्तेमाल में, विधि व्यवसाय करने का किसी अधिवक्ता का अनुज्ञप्ति-पत्र इसके द्वारा निरस्त या निलम्बित हो सकता है किन्तु इस विनिश्चय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, AIR 1998 SC 1895 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 (2) से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि. अवमान की अधिकारिता संसद के द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत होती है। संसद ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को अधिनियमित किया है, जिसने बार कौंसिल को किसी अधिवक्ता के विधि-व्यवसाय करने के अनुज्ञप्ति-पत्र को धारा 38 के परन्तुक के द्वारा अपेक्षित नोटिस देने के बाद अवमान करने वाले अधिवक्ता को व्यावसायिक रूप से दण्डित करने के लिए दण्ड के तौर पर उसके अनुज्ञप्ति-पत्र को निरस्त या निलम्बित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। धारा 38 के अन्तर्गत अपीलीय शक्ति मात्र सर्वोच्च न्यायालय को मिली है, हाईकोर्ट को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी हाईकोर्ट के साथ-ही-साथ सर्वोच्च न्यायालय अवमान करने वाले अधिवक्ता की अपने सामने उपस्थित होने के लिए उस समय तक रोक सकता है, जब तक कि वह अवमान से अपने आपको स्वतंत्र नहीं कर लेता है।
प्रश्न 40. विधि स्नातक । Law Graduates.
उत्तर-विधि स्नातक (Law Graduates) – अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (ज) “विधि स्नातक” शब्द को परिभाषित करती है। “विधि स्नातक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।
प्रश्न 41. राज्य नामावली। State role.
उत्तर- राज्य नामावली (State Role) – अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (ढ़) में “राज्य नामावली” से तात्पर्य धारा 17 के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार की गई और रखी गयी अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ताओं की ऐसी नामावली तैयार करेगी और रखेगी जिसमें अधिवक्ताओं के दो भाग होंगे-प्रथम भाग में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम एवं पते होंगे और दूसरे भाग में अन्य अधिवक्ताओं के नाम होंगे।
प्रश्न 42. नामांकन प्रमाण पत्र। Certificate of enrolment.
उत्तर- नामांकन प्रमाण पत्र (Certificate of Entrolment)- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 22 यह प्रावधान करती है कि राज्य विधिज्ञ परिषद् प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन उसके द्वारा रखी गई नामावली में दर्ज है, विहित प्ररूप में नामांकन प्रमाणपत्र जारी करेगी। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम राज्य नामावली में इस प्रकार दर्ज है, अपने स्थायी निवास स्थान में किसी परिवर्तन की सूचना सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसे परिवर्तन के 90 दिन के भीतर देगा।
प्रश्न 43. विधि का शासन। Rule of Law.
उत्तर- विधि की सर्वोच्चता विधि के शासन की स्थापना के लिए एक आवश्यक शर्त है। विधिक शोषण का अर्थ है, मनमानी करने की शक्ति के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता अथवा प्रधानता विधि का शासन मनमानेपन विशेषाधिकार अथवा विस्तृत वैवेविक प्राधिकार के अस्तित्व का अपवर्जन करती है। किसी व्यक्ति को तभी दण्डित किया जा सकता है जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया हो। इसका यह भी अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं अथवा साधारण विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित देश की सामान्य विधि द्वारा सभी वर्गों को सम्यक् अधीनता। विधि का रासन यह तथ्य व्यक्त करने के सिद्धान्त के रूप में प्रयुक्त हो सकता है कि सांविधानिक विधि न्यायालय द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित व्यक्तियों की नियमित कार्यकलापों का परिणाम है न कि इसका स्रोत। इसका तात्पर्य यह भी है कि संविधान देश की सामान्य विधि का परिणाम है। किन्तु भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान की सर्वोच्चता है।
प्रश्न 44. क्या बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश अपील योग्य होता है? स्पष्ट कीजिए ?
Where the order passed by the Disciplinary Committee of Bar Council of India appealable? Explain.
उत्तर- बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य होते हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा धारा 36 या धारा 37 के अधीन या यथास्थिति भारत के महान्यायवादी या सम्बद्ध राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिये गये आदेश कथित कोई व्यक्ति उस तारीख से साठ दिनों के भीतर जिसको उसे वह आदेश संसूचित किया जाता है, उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय उस पर ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड में परिवर्तन करने का आदेश भी है, पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1973 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India) का अनुशासन समिति का कोई भी आदेश कथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जायेगा जिससे कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
प्रश्न 45. क्या भारत के महान्यायवादी को अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार है? स्पष्ट कीजिए।
Whether the Attorney General of India have the right of preaudience over all other Advocates?
उत्तर- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को सम्पूर्ण भारत में सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार है। इस अधिनियम में अवरोही क्रम में पूर्व सुनवाई का उत्क्रमात्मक अधिकार का प्रावधान किया गया है। धारा 23 (1) के अनुसार भारत के महान्यायवादी की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी जिसमें सालिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी शामिल है। धारा 23 (2) के अनुसारे भारत के महान्यायवादी को छोड़कर अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व भारत के सालिसिटर जनरल की सुनवाई होगी।
इसी प्रकार से अधिनियम की धारा 23 (5) के अंतर्गत यह विधान किया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व होगी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में परस्पर और अन्य अधिवक्ताओं में परस्पर पूर्व सुनवाई का अधिकार उनकी अपनी-अपनी ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित किया जायेगा।
इस प्रकार से उत्क्रमात्मक आधार पर भारत का महान्यायवादी जो सर्वोच्च सरकारी अधिवक्ता होता है, को भारत के सरकारी एवं गैर सरकारी सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
प्रश्न 46. क्या किसी अधिवक्ता के लिए अपना विज्ञापन करना प्रतिषिद्ध है? स्पष्ट कीजिए।
Whether self advertisement for a lawyer forbided. Discuss.
उत्तर- वस्तुतः अधिवक्ताओं को स्वयं का विज्ञापन करने से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है। विधिक व्यवसाय का यह सुस्थापित नियम है कि स्वयं का विज्ञापन करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे वृत्तिक अवचार माना जायेगा और वृत्तिक शिष्टाचार का भंग भी समझा जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि विधि व्यवसाय कोई उद्योग अथवा व्यापार नहीं है अतः स्वयं द्वारा किसी भी प्रकार के विज्ञापन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। किसी अधिवक्ता के लिए निश्चित रूप से यह अच्छा अस्परण नहीं है कि वह संभावित मुवक्किलों को फँसाना या पटाना प्रारम्भ कर दे। यह पहले ही अनुभव किया जा चुका है कि किसी अधिवक्ता के पास काम उसके ज्ञान, निष्ठा, ईमानदारी एवं उचित व्यवहार पर आता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल से बात-व्यवहार का तरीका विज्ञापन का सबसे सशक्त तरीका है। इंग्लैण्ड में किसी अधिवक्ता द्वारा स्वयं के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने की बात पर यह प्रकाश डाला गया है कि प्रकाशन के लिए अधिवक्ता का हस्ताक्षरित फोटोग्राफ तक देना अव्यावसायिक समझा जाना चाहिए।
प्रश्न 47. किन मामलों में अवमानना दण्डनीय नहीं होती है?
What are the cases where contempt is not punishable?
उत्तर – न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन न्यायालय अवमान के लिए कोई दण्डादेश तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान न हो जाय कि अवमानना इस प्रकार की है कि वह न्याय के सम्यक् अनुरूप में या तो सारभूत रूप से हस्तक्षेप करती है, या सारभूत रूप से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है।
न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 के उपर्युक्त प्रावधान का यह तात्पर्य है कि कतिपय मामलों में अवमानना के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता है अर्थात् यदि न्यायालय इस बात पर संतुष्ट हो जाय कि इस प्रकार की अवमानना की प्रवृत्ति वस्तुतः ऐसी है कि इससे न्याय के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की कार्यवाहियों की स्वच्छता पूर्वक रिपोर्टिंग करना, न्यायिक उद्घोषणाओं की समालोचना करना, न्यायालय के समक्ष तार्किक बहस करना और न्यायालय की कार्यवाहियों के दौरान न्यायपूर्ण एवं उचित आपत्तियाँ उठाना न्यायालय की अवमानना की कोटि में नहीं आता है। निःसंदेह किसी विधिज्ञ (अधिवक्ता) को न्यायालय के समक्ष भाषण करने का असीमित विस्तार क्षेत्र प्राप्त होता है किन्तु इसे सुसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित होना चाहिए तथा इसका उद्देश्य न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए।
प्रश्न 48. कार्यकारिणी समिति। Executive Committee.
उत्तर- कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)– अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10 (1) (क) में राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा स्थायी समितियों में एक कार्यकारिणी समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित पाँच सदस्यों से मिलकर बनेगी। जबकि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति में परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित भी सदस्यों से मिलकर बनेगी।
प्रश्न 49. विशेष समिति का गठन। Constitution of Special Committee.
उत्तर- विशेष समिति का गठन (Constitution of Special Committee)- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 (क) चुनाव की अनुपस्थिति में विशेष समिति के गठन का प्रावधान करती है। जहाँ एक राज्य विधिज्ञ परिषद् पाँच वर्षों की अवधि या वर्धित अवधि की समाप्ति के पूर्व, इनके सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करने में असफल हो जाता है, वहाँ भारतीय विधिज्ञ परिषद् ऐसी समाप्ति के दिन की तत्काल तिथि से निम्न में से एक विशेष समिति का गठन करेगा।
(i) अध्यक्ष होने के लिए धारा 3 की उपधारा (2) (क) में विनिर्दिष्ट किये गये राज्य अधिवक्ता परिषद् के पदेन सदस्य; परन्तु जहाँ एक से ज्यादा पदेन सदस्य होते हैं, वहाँ उनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा; और
(ii) दो सदस्यों का राज्य विधिज्ञ परिषद् के चुनावी अनुक्रमांक पर अधिवक्ताओं के बीच में से भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा। राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्यों का उन्मोचन करेगा जब तक अधिवक्ता संघ का इस अधिनियम के अधीन गठन नहीं किया जाता है।
विशेष समिति के गठन पर और जब तक इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता संघ का गठन नहीं कर दिया जाता है-
(क) राज्य विधिज्ञ परिषद् में निहित होने वाली सभी सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ, विशेष समिति में निहित होंगी।
(ख) राज्य विधिज्ञ परिषद् के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएँ चाहे किसी संविदा से उद्भूत हुई हों अथवा अन्यथा, विशेष समिति का अधिकार, दायित्व एवं बाध्यताएँ होंगी।
प्रश्न 50. विधिक परामर्श। Legal Advice.
उत्तर-विधिक परामर्श (Legal Advice) – विधिक परामर्श से तात्पर्य विधिक जानकारी उन लोगों को प्रदान करना जिन्हें जानकारी के अभाव में न्याय नहीं मिल पा रहा है। विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्धनों के लिए विधिक सहायता और सलाह देने के लिए आयोजन और उस प्रयोजन के लिए समितियों और उपसमितियों का गठन और उनके कृत्य तथा उन कार्यवाहियों का विवरण जिनके सम्बन्ध में विधिक सहायता या सलाह दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में नियम बना सकेगी। (धारा 15)
प्रश्न 51. नामांकन के लिए निरर्हता। Disqualification for enrolment.
उत्तर- नामांकन के लिए निरर्हता- अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 (क) यह उपबन्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा, यदि-
(क) वह नैतिक अधमता से सम्बन्धित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;
(ख) वह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।
परन्तु नामांकन के लिए यथापूर्वोक्त निरर्हता, उसके निर्मुक्त होने से दो वर्ष की अवधि की सम्माप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगी।
इस धारा का कोई भी उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है। इण्डियन कौंसिल ऑफ लीगल एड एण्ड एडवाइस बनाम बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० 1995 एस० सी० 691 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् का नियम जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से वर्जित करता है, उसकी शक्ति से परे होने के कारण शून्य है।
Adv. Prem Kumar Nigam
Mob. 9758516448