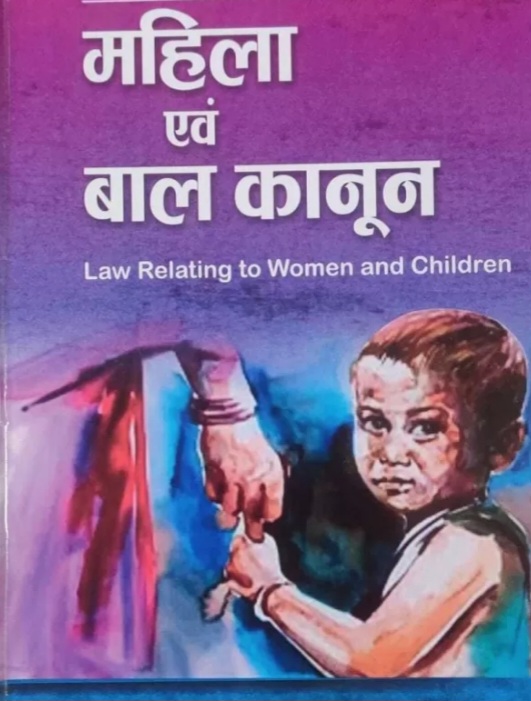संयुक्त राष्ट्र अभिसमय तथा महिलाओं एवं बालकों से सम्बन्धित भारतीय विधि (U.N. Conventions and Indian Law Relating to Women and Children)
प्रश्न 1. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1979 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। Explain the main features of the International convention on elimination of all forms of discriminations against women, 1979.
उत्तर- पुरुष एवं स्त्री इस सृष्टि की एक महत्त्वपूर्ण रचना है। सृष्टि की रचना के लिए इन दोनों का होना नितान्त जरूरी है। स्त्री केवल सृष्टि की रचना ही नहीं करती है बल्कि वह बच्चे को जन्म देने के साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की ओर भी ध्यान देती है। वह बच्चे का उचित रूप से लालन-पालन करती है और एक देश के भविष्य का निर्माण करती है। उसकी महत्ता को समझते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किये जाते हैं।
लिंग के आधार पर न्याय सभी से सम्बन्धित है। इसके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई विश्व सम्मेलन प्रायोजित किये गये। महासभा द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध भेदभावों की समाप्ति पर घोषणा को 7 नवम्बर, 1967 को अंगीकार किया गया तथा इसके सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए महासभा द्वारा 18 दिसम्बर, 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति पर अभिसमय अंगीकार किया गया, जो कि वर्ष 1981 में लागू हुआ। वर्ष 1993 में भारत द्वारा इसे अनुसमर्थित किया गया। वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाना इसका महत्व दर्शाता है।
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव (Discrimination Against Women)— हालांकि मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक महिलाओं के साथ-साथ सभी व्यक्तियों के अधिकारों की विस्तृत रूप में चर्चा करता है, परन्तु महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय आवश्यक समझे गये अभिसमय को उद्देशिका के अनुसार महिलाओं को अभी भी पुरुषों के समान अधिकार नहीं हैं। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाज में व्याप्त है।
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का अर्थ लिंग के आधार पर किया गया है। ऐसा कोई भेद अपवर्जन या प्रतिबन्ध है, जिसका प्रभाव अथवा उद्देश्य महिलाओं की पारिस्थिति पर बिना विचार किये हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिविल या अन्य किसी क्षेत्र में महिलाओं की मान्यता पर पड़ता हो या उनके द्वारा मानव अधिकारों या मौलिक अधिकारों के उपभोग पर पड़ता हो। [अनुच्छेद-1] अभिसमय के पक्षकारों ने महिलाओं के विरुद्ध सभी रूपों में भेदभाव की भार्त्सना की है और हर सम्भव साधन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं, तथा इस लक्ष्य प्राधि के लिए उन्होंने-(क) पुरुष एवं महिलाओं की समन के सिद्धान्त को अपने राष्ट्रीय संविधान अथवा अन्य उपयुक्त विधानों में यदि यह सिद्धान्त उनमें पहले से शामिल न हो, तो इसे शामिल करने, (ख) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को प्रतिषेध करते हुए उपयुक्त विधायी एवं अन्य उपायों को अंगीकार करने, (ग) पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं के अधिकारों के विधिक संरक्षण की स्थापना, (घ) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के किसी कार्य अथवा अभ्यास में संलग्न होने से विरत रहने, (ङ) किसी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्त करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाने, (च) देश के सभी दाण्डिक उपबन्ध, जिनसे कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव होता हो, की निरसित करने का वचन दिया है।
कार्यान्वयन – अभिसमय के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अभिसमय के प्रावधानों के कार्यान्वयन में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार करने के उद्देश्य से, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर समिति (CEDAW) की स्थापना के लिए प्राविधान किया गया। इस समिति में 18 सदस्य (अभिसमय के प्रवर्तन के समय) तथा 23 सदस्य (पैंतीस राज्यों द्वारा अभिसमय के अनुसमर्थन अथवा स्वीकृति के पश्चात्) होंगे। इसके सदस्यगण उच्च नैतिक स्तर के विशेषज्ञ होंगे और उन्हें अभिसमय द्वारा समावेश किये गये क्षेत्र में क्षमता प्राप्त होगी। विशेषज्ञों का निर्वाचन राज्य पक्षकारों द्वारा अपने राष्ट्रिकों के बीच से किया जायेगा और वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर कार्य करेंगे।
राज्य पक्षकार निश्चित समय पर समिति को विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक अथवा अन्य ऐसे उपायों की रिपोर्ट देंगे जिन्हें उन्होंने अभिसमय के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अंगीकार किया है। समिति के क्रिया-कलापों पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के माध्यम से महासभा को वार्षिक रिपोर्ट देगी तथा रिपोर्ट में परिक्षण एवं राज्य पक्षकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित सुझाव देगी और सामान्य सिफारिश करेगी।
अभिसमय के लागू होने के उपरान्त महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के सम्बन्ध मैं एक समिति वर्ष 1981 में बनायी गयी, जिसके 23 स्वतन्त्र विशेषज्ञ हैं। समिति की बैठक केवल 2 सप्ताह के लिए होती है जो कि स्पष्टतः अपर्यास है। राज्य पक्षकार निश्चित समय पर समिति को विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक अथवा अन्य उपायों की रिपोर्ट देंगे। इस प्रकार अभिसमय का कार्यान्वयन राज्यों की रिपोर्ट के द्वारा होता है।
महिलाओं पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकाल – अभिसमय में व्यक्तिगत शिकायत की स्थापना नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए 7 अक्टूबर, 1999 को महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेद-भावों की समाप्ति पर अभिसमय का वैकल्पिक प्रोटोकाल अंगीकार किया, जिसके अनुसार लिंग भेद, यौन शोषण एवं अन्य अपधाराओं से पीड़ित महिलायें व्यक्तिगत रूप से समिति को अपनी शिकायत भेज सकती हैं. तथा समिति इस बारे में अन्वेषण कर सकती है। 21 अनुच्छेदों का यह प्रोटोकाल उस समय लागू होगा जब इसे 10 (दस) राज्यों द्वारा समर्थन मिल जायेगा। 7 सितम्बर, 2000 तक प्रोटोकाल के 9 (नौ) राज्य पक्षकार थे। प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लिखित रूप से समिति की सूचना दे सकता है, परन्तु शिकायतकर्ता गुमनाम नहीं हो सकता। सूचना प्राप्त होने पर समिति राज्य पक्षकार से निवेदन कर सकती है कि वह तथा कथित पीड़ित व्यक्ति को अपूर्णीय क्षति से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। राज्य पक्षकार को शिकायत के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए 6 (छह) मास का समय दिया जाता है। समिति के सुझाव सम्बन्धित पक्षकारों को भेद दिये जाते हैं। राज्य पक्षकार को समिति के सुझाव पर विचार करने तथा किये गये उपायों के सम्बन्ध में लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट करने के लिए छह मास का समय दिया जाता है।
प्रोटोकाल के अनुसार अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों का राज्य पक्षकार द्वारा उल्लंघन करने के सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर समिति अपने सदस्यों द्वारा गोपनीय अन्वेषण करा सकती है। समिति राज्य पक्षकार की सहमति से आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र का निरीक्षण कर सकती है। समिति अपना निष्कर्ष, समीक्षा या सुझाव राज्य पक्षकार को भेज देती है। छह महीने के उपरान्त राज्य पक्षकार को किये गये उपायों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।
यह सम्मेलन और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति पर अभिसमय, वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में स्त्रियों के मानवाधिकारों का अनेक प्रकार से उल्लंघन हो रहा है।
प्रश्न 2. बदलते समाज में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। Explain the Status of the women in a changing society.
उत्तर- वर्तमान युग की नारी अनेक युगों से होकर गुजरी है। विभिन्न कालों एवं युगों में उनकी स्थिति भी बदलते समाज के अनुसार बदलती रही है।
वैदिक युग – वैदिक युग में नारी की स्थिति अत्यन्त गौरवशाली रही है। उस युग में नारी को समानता का दर्जा प्राप्त था और वह स्वतन्त्र थी। जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सह भागीदारी रहती थी। वह गुरुकुल में अध्ययन करती थी। अपाला, गार्गी, यामिनी आदि ऐसी कुछ नारियाँ थीं जिनका समाज में अपना एक अलग ही मुकाम था। उस समय की नारी कला, साहित्य एवं संस्कृति में निपुण होती थीं। महाभारत में नारी को सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नारी के बिना कोई भी समारोह सम्पन्न नहीं हो सकता था। वैदिक काल के पश्चात् नारी की स्थिति में कुछ बदलाव आया। परिवार एवं समाज में उसके स्थान को थोड़ा आघात लगा। उस समय नारी को अनेक यातनायें एवं उपहास का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे यह स्थिति भी बदली और अब नारी को स्त्री धन जैसे अधिकार मिलने लगे।
मध्य युग– मध्य युग में नारी की स्थिति काफी बिगड़ गयी। परिवार एवं समाज में वह उपहास एवं उपेक्षा की पात्र बनीं। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों से उसे वंचित रखा गया। बाल-विवाह, दहेज, देव दासी, बहुविवाह, सतीप्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं ने जारी का अत्यधिक शोषण किया।
ब्रिटिश काल- ब्रिटिश काल में नारी जाति के उत्थान के लिये अनेक प्रयास किये गये। पुरुष एवं नारी के बीच समानता, स्वतन्त्रता आदि की अवधारणा का प्रादुर्भाव इसी काल में माना जाता है। उस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के आन्दोलन चले-
(1) समाज सुधार अन्दोलन, एवं
(2) राष्ट्रवादी आन्दोलन।
समाज सुधार आन्दोलन 19वीं शताब्दी के दौरान चला, जिसके अन्तर्गत महिलाओं की समान स्थिति का प्रश्न उठाया गया। उस समय सती, पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध, सम्पत्ति के अधिकार से महिलाओं का वंचित होना, बाल विवाह, नारी शिक्षा आदि अनेक समस्यायें व्याप्त थीं। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिये स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, एनी बेसेन्ट आदि ने अनेक आन्दोलन चलाये। स्वयं महात्मा गाँधी ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध, देवदासी प्रथा आदि की खुलकर आलोचना की। सन् 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेन्स का गठन किया गया। महिलाओं की ओर से समानता के अधिकार की माँग उठाई गई। जिसके परिणामस्वरूप विधायिका द्वारा अनेक अधिनियम पारित किये गये-
(1) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
(2) बाल-विवाह निषेध अधिनियम,
(3) हिन्दू महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम, आदि।
इसके साथ ही साथ औद्योगिक कानूनों में भी महिलाओं एवं बालकों के लिए व्यापक सुधार किये गये। इनके रात्रिकालीन नियोजन को निषेधित किया गया।
इसके साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये एवं उन्हें समानता का दर्जा देने के लिये कई नारी आन्दोलन भी चलाये गये। जैसे- (i) उदारवादी आन्दोलन, (ii) अग्र आन्दोलन, (iii) समाजवादी आन्दोलन।
उदारवादी आन्दोलन 18वीं शताब्दी में चला। जिसके अन्तर्गत महिलाओं की दयनीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया और यह कहा गया कि महिलायें भी मानवीय प्राणी हैं। वे मात्र भोग-विलास की वस्तु नहीं हैं। उनके भी अपने मानवाधिकार हैं।
सन् 1969 से 1970 के दौरान उग्र आन्दोलन चला, जिसमें लिंग विभेद का व्यापक विरोध किया गया। महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा, काम, वेतन आदि दिये जाने की माँग की गई। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचारों का भी खुलकर विरोध किया गया। पुनः कालान्तर में समाजवादी आन्दोलन चला। जिसका मुख्य उद्देश्य एक समाजवादी समाज की संरचना करना था। इस आन्दोलन का सती निवारण, बाल-विवाह निषेध, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध, नारी स्वातन्त्र्य आदि से भी सरोकार रहा।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलायें – नारी स्वातंत्र्य का मिशन केवल राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं होकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छाया रहा। समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों, नारी स्वतन्त्रता तथा मानवाधिकार पर अनेक बार अधिवेशन बुलाये गये तथा अभिसमय पारित किये गये-
(1) मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घेषणा 1948
(2) महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर अभिसमय, 1953
(3) विवाहित महिलाओं को राष्ट्रीयता पर अभिसमय, 1957
(4) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन की घोषणा, 1967.
(5) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के समापन पर अभिसमय, 1979
(6) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर अभिसमय, 1993
(7) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय का स्वैच्छिक प्रोटोकाल 1999
(8) महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग आदि।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में महिलाओं के अनेक अधिकारों को स्थान दिया गया। इसमें लिंग, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना प्रत्येक महिला को विवाह करने और परिवार का गठन करने का अधिकार दिया गया। इसके अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र एवं समान अधिकारों के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार है।
महिलाओं के सिविल, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर भी समय-समय पर अभिसमय बने और इन अभिसमयों में महिलाओं के लिये-
1. शिक्षा,
2. सामाजिक सुरक्षा,
3. नियोजन,
4. सांस्कृतिक जीवन में भागीदरी,
5. सम्पत्ति धारण करने की क्षमता,
6. विवाह करने एवं परिवार बसाने का अधिकार,
7. दासता से मुक्ति का अधिकार आदि के बारे में प्रावधान किया गया।
सन् 1946 से महिलाओं की प्रास्थिति पर एक आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर जाँच कर अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा। सन् 1975 में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करने के लिये मैक्सिको सिटी में वियना कॉन्फ्रेन्स बुलाई गई जिसमें महिलाओं के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, समानता एवं शान्ति पर विचार किया गया। इसी प्रकार सन् 1995 में चीन में बीजिंग कॉन्फ्रेन्स बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेन्स में भी महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। जनवरी, 2002 में काठमांडू में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया, जो महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा के लिये महत्वपूर्ण रहा।
इस प्रकार विभिन्न युगों और कालों में प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलओं की भिन्न-भिन्न स्थिति रही। प्रत्येक काल में महिलाओं के उन्नयन और उत्थान की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये। आज नारी न केवल पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है अपितु वह सुरक्षित भी है। अनेक विधियों और संविधान में महिलाओं से जुड़े अधिकारों के बारे में व्यापक प्रावधान किये गये हैं। आपराधिक विधियों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।
समाज में भी अब नारी को पुनः श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब यह कहा जाने लगा कि-
‘नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद, नभ तल में, पियूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में’
इस प्रकार देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप नारी का स्वरूप भी बदल गया। अब नारी एक नये परिवेश में हमारे समक्ष हैं। अब लिंग भेद अर्थात् पुरुष एवं नारी में किसी प्रकार का विभेद नहीं रह गया है। नारी अब पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी है। कर्म क्षेत्र में भी नारी अग्रिम पंक्ति में है। हमारे संविधान में नारी को पुरुष समकक्ष ही नहीं अपितु एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है।
प्रश्न 3. बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में उल्लिखित अधिकारों की व्याख्या कीजिए। Explain the different rights of children enshrined under the Child Rights United Nations Convention.
उत्तर – बालकों से सम्बन्धित कानून भी समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल का मनुष्य वैसा ही होगा जैसा कि वह आज बच्चे के रूप में है। जब हम बालकों के अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के विषय में चर्चा करते हैं जो कि अपने अधिकारों को व्यक्त भी नहीं कर सकता और अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। यदि वह कुछ कहता है तो लोग उसके कथन को मान्यता नहीं देते क्योंकि वह अवयस्क है। यह समझा जाता है कि वह अपने हित के बारे में नहीं जानता है। इसलिए उसके अधिकारों को समझना तथा उसकी रक्षा करने का दायित्व वयस्कों पर होता है।
वर्ष 1924 में शिशु के अधिकारों पर जेनेवा उद्घोषणा अंगीकार किये जाने के साथ ही लोग ऑफ नेशन्स के द्वारा इस सम्बन्ध में शुरुआत की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिशु के अधिकारों पर दूसरी उद्घोषणा अंगीकार करते हुए वर्ष 1959 में प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की। तदुपरान्त वर्ष 979 अन्तर्राष्ट्रीय बालक वर्ष के रूप में मनाया गया। 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र शिशु के अधिकारों पर अभिसमय को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया जो कि 2 सितम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ। वर्ष 1992 में भारत ने इसे अनुसमर्थित किया। केवल इतना ही नहीं नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराध के मामलों में महिलाओं एवं बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए 17 जुलाई, 1998 को रोम में अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विशेष सत्र में 11 मई, 2002 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा हेतु एक एजेंडा”ए वर्ल्ड फिर फार चिल्ड्रेन” अनुसमर्थित किया गया। ऐसा पहला विशेष सत्र था कि जिसमें बालकों की समस्याओं को उन्हीं से सुना गया। भारतवर्ष में भी स्व: पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष, बच्चों के प्रति उनके अपार प्रेम के कारण ‘बालक दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को जो संयुक्त राष्ट्र शिशु के अधिकारों पर अभिसमय को अंगीकार किया गया है इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 के अनुसार 18 साल से कम आयु के सभी व्यक्तियों के साथ शिशु अथवा बालक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जब तक कि सदस्य देशों को विशिष्ट विधियों के अन्तर्गत वयस्कता शीघ्र न प्राप्त होती हो। “शिशु की परिभाषा विभिन्न श्रम विधियों, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम तथा शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित विधियों में भिन्न हो सकती है।
अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं और यह तीन भागों में विभाजित है।
शिशु के अधिकार (Rights of the Child) – अभिसमय में शिशुओं के बहुत से अधिकार दिये गये हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
(1) प्राण का अधिकार (Right to Life)- अभिसमय के अनुच्छेद 6 परिच्छेद 1 के अनुसार एक शिशु को प्राण या जीवन का अन्तर्निहित अधिकार हैं। इस प्रकार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किये गये अपराध के लिए मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा के अनुच्छेद 6 (5) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराध के लिए मृत्युदण्ड से दण्डित नहीं किया जायेगा तथा किसी महिला को गर्भावस्था की अवधि में मृत्युदण्ड नहीं दिया जायेगा।
यह एक आत्यान्तिक या स्पष्ट अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में इसका अपवाद नहीं होना चाहिये। जीवन का अधिकार का होना यह इंगित करता है कि जिन्दगी भर के लिए सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि कारागार में व्यतीत किया गया जीवन कोई मायने नहीं रखता।
(2) नाम का अधिकार (Right to Name) — अभिसमय के अनुच्छेद 7 (1) के अनुसार शिशु को नाम का अधिकार है। यह नाम सम्मानजनक होना चाहिए।
किसी व्यक्ति का नाम या पदवी उसके आचरण को प्रभावित करता है। कुछ स्मृतियों के अनुसार शूद्रों के बच्चों का तिरस्कृत नाम होना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार- ब्राह्मणों के नाम का प्रथम भाग शुभ, मंगलदायक होना चाहिए लेकिन एक शूद्र का तिरस्कृत होना चाहिए।
एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग प्रसन्नतादायक होगा, एक क्षत्रिय का संरक्षण देने वाला एक, वैश्य का विकासशील या सफलतादायक और एक शूद्र का सेवा से सम्बन्धित होना चाहिए।
इस प्रकार हमें ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं जो कि एक संवेदी विचारशील व्यक्ति द्वारा उचित नहीं समझे जा सकते जैसे-लोभीलाल, जंगली, दुखिया एवं कचरादेयी आदि। ऐसे नाम एक युक्तियुक्त व्यक्ति के लिए कष्टदायी हैं और उन्हें ऐसे नामों से नहीं पुकारा जाना चाहिए।
(3) माता-पिता द्वारा देखभाल का अधिकार – अभिसमय के अनुच्छेद 9 (1) के अनुसार माता-पिता द्वारा शिशु की देखभाल किया जाना चाहिए। इस प्रकार माता-पिता दोनों के द्वारा या दोनों में किसी एक के द्वारा प्रतिदिन यथोचित समय शिशु को देना आवश्यक है। पति तथा पत्नी दोनों लोगों के द्वारा नौकरी करने से उनके बच्चे इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। ब्रिटेन में 5 से 10 वर्ष की आयु के लगभग 8 लाख शिशुओं को स्कूल समय के बाद पूरी तरह से अकेले व्यतीत करना पड़ता है। माता-पिता दोनों ही कार्य करने के स्थान पर होते हैं।
शिशु कक्ष की फीस या शुल्क का भुगतान करना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए सरकार चिन्हित है क्योंकि ऐसे बालक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते।
भारतवर्ष में भी आर्थिक समस्या के करण पति एवं पत्नी दोनों ही करना पसन्द कर रहे हैं। इस प्रकार उन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है और संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त होने के कारण परिवार का कोई सदस्य बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं होता।
(4) स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) – अभिसमय के अनुच्छेद 24 (1) के अनुसार शिशु को स्वास्थ्य का अधिकार है। उसके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिशु को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त स्तर के उपभोग तथा बीमारी के उपचार एवं स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हेतु सुविधाओं का अधिकार है।
(5) बाल श्रम (Child Labour)- अभिसम के अनुच्छेद 32 (1) के उपबन्धों के अनुसार शिशु को आर्थिक शोषण से संरक्षण का अधिकार है। बालक को ऐसे कार्यों से संरक्षण का अधिकार है जो कि जोखिम से परिपूर्ण या जो शिक्षा ग्रहण करने में विघ्न उत्पन्न करते हो या जो कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक या नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो।
यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि माता-पिता खर्च वहन कर सकते तो वे अपने बच्चों को काम पर न भेजकर स्कूल अवश्य भेजते। आर्थिक तंगी होने के कारण बाल श्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता। बालक अपने तथा परिवार के लिए कार्य करने जाते हैं यदि कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है।
यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि नियोजक सभी बाल श्रमिकों को हटा दें तो वे बर्बाद हो जायेंगे तथा वेश्यावृत्ति या अपराध में लिप्त हो जायेंगे या और भी कम वेतन पर कार्य करने के कारण दशा बदतर हो जायेगी। बाहर घूमने वाले बच्चों को पुलिस, सरकार एवं निजी सुरक्षा बल सभी परेशान करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बच्चों से अधिक काम क्यों लिया जाता है? कार्य करने का स्थान अस्वास्थ्यकर क्यों होता है? कारखानों में जबरजस्ती काम लेने के लिए बच्चों का व्यपहरण क्यों किया जाता है।
(6) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)— बालकों के अधिकारों पर अधिनियम, 1989 द्वारा अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत प्रत्येक बालक की शिक्षा के मूल अधिकार को अभिस्वीकृति प्रदान की गयी है। विशेषकर सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाये जाने के लिए राज्य पर दायित्व डाला गया है। यह अनुच्छेद पढ़ाई के बीच में हो विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की दर में कमी लाने के लिए कदम उठाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के बावजूद अर्थात् सभी बालकों को उनके द्वारा 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के राज्य पर समयबद्ध दायित्व को निर्दिष्ट करने की नीति निर्देशित सिद्धान्त के होते हुए भी शिक्षा का अधिकार अभी भी पुनर्गठित नहीं हो पाया है। यही कारण है। आजादी के पाँच से भी अधिक दशक व्यतीत होने के बाद भी, व्यापक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी काफी लम्बी दूरी तय करनी है।
देश भर में इस समय ऐसी कोई समरूप संहिता लागू नहीं जो प्रारम्भिक स्तर तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के गारण्टी दे तथापि कतिपय राज्य विधानों जैसे कि दिल्ली प्राइमरी शिक्षा अधिनियम, 1960 में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए वैधानिक ढंग से व्यवस्था की गयी है। अधिनियम में उपस्थित प्राधिकारियों की नियुक्ति परिकल्पित की गयी है जो माता-पिता के बालकों को विद्यालय भेजने के उत्तरदायित्व को अधिसूचित करने के लिए आबद्ध है। इस अधिसूचना के अनुपालन में किसी भी प्रकार की असफलता जुर्माने से दण्डनीय होगी।
उन्नीकृष्णन जे० पी० व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० ए० आई० आर० (1993) एस० सी० 2178, के बाद में हाल में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्राथमिक शिक्षा को वैयक्तिक स्वतन्त्रता के पहलु के रूप में मान्यता दी गयी है और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रत्येक बालक के संवैधानिक अधिकार के स्तर तक उठाया है।
इस सम्बन्ध में न्यायमूर्ति बी० पी० जीवन रेड्डी का निम्नलिखित सम्प्रेक्षण अत्यन्त प्रासंगिक है- “शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 द्वारा गारण्टीकृत जीवन एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार में विवक्षित है, संविधान के भाग IV में निर्देशित सिद्धान्तों के प्रकाश में अर्थान्वित किया जाना आवश्यक है, भाग IV में अनेक अनुच्छेद हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया गया है।” अनुच्छेद 41 में यह बताया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता. एवं विकास की सीमाओं के भीतर कार्य, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी तथा निर्योग्यता के मामलों में तथा अनुचित अभाव के अन्य मामलों में लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी उपबन्ध करेगा।
अनुच्छेद 45 में यह बताया गया है कि राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर, प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 46 में आदेशित है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु विशेष ध्यान देगा तथा उनको सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा करेगा। शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान से है तथा “ज्ञान स्वयं शक्ति है।” जैसा जॉन एडम द्वारा ठीक ही सम्प्रेक्षित किया गया है। पंक्तियों में ज्ञान के साधनों का परिरक्षण लोगों के लिए देश के सभी धनी व्यक्तियों की सम्पत्ति से कहीं अधिक महत्व होता है। यह बात अनुच्छेद 46 में भली-भाँति पिरोई गयी प्रतीत होती है। यह केवल निष्ठुर शासन तथा अमान्य नियम ही है जो शिक्षा के विस्तार से भयभीत हैं। उन्होंने कहा, “सर्वाधिक शिक्षा सबसे अधिक नाशकारक एवं विघटनकारी विष है जिसे उदारवाद ने स्वयं अपने विनाश के लिए खोज निकाला है।” सच्चा जनतन्त्र वही होता है जहाँ शिक्षा व्याप्त होतो है, जहाँ लोग यह समझते हैं कि उनके तथा राष्ट्र के लिए क्या सही है और यह जानते हैं कि स्वयं को कैसे शासित किया जाय। अन्य लक्ष्यों के साथ उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीन अनुच्छेदों 45, 46 एवं 41 को तैयार किया गया है।
अन्तिम रूप से, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि – “राज्य को अनुच्छेद 45 के आदेश का सम्मान करना चाहिए। कम से कम अब तो इसे वास्तविकता में तब्दील किया जाना चाहिए। निःसन्देह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 45 के वचन को इस शताब्दी की समाप्ति के पूर्व विमोचित किया जायेगा। चाहे जैसी भी दशा हो, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी बालक को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार है।
उत्तर प्रदेश राज्य ने अब तक उस अनिवार्य शिक्षा विधान को अधिनियमित नहीं किया है जो 14 राज्यों एवं 4 केन्द्रशासित प्रदेशों में विद्यमान हो उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1972 में स्पष्ट रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसे अभी भी वैधानिक मान्यता की प्रतीक्षा है।
अभिसमय के द्वारा शिशु को कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं-
(1) राष्ट्रीयता अर्जित करने का अधिकार (अनुच्छेद 7)
(2) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार ( अनुच्छूद 13, परिच्छेद 1)
(3) विचार अन्तःकरण एवं धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 14, परिच्छेद 1)
(4) संगम की स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण सभा करने का अधिकार ( अनुच्छेद 15, परिच्छेद 1)
(5) सामाजिक सुरक्षा से लाभ का अधिकार (अनुच्छेद 26, परिच्छेद 1)
(6) शिशु के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्यिक एवं सामाजिक विकास हेतु पर्याग जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 27 परिच्छेद 1)
(7) शिशु की एकान्तता, परिवार गृह या पत्राचार में मनमाना एवं विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध विधि संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 16 परिच्छेद 1 ) ।
शिशु अधिकार समिति (Committee on the rights of child) वर्ष 1991 से अभिसमय के उद्देश्यों का अनुश्रवण कर रही है। अभिसमय के अनुच्छेद 43 के अनुसार उच्च नैतिक स्तर एवं मान्य क्षमता वाले 10 (दस) विशेषज्ञ उसके सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होगा और वे पुनः चुनाव के योग्य होंगे। अभिसमय के राज्य पक्षकारों के सम्मेलन में 12 दिसम्बर, 1995 को अनुच्छेद 43 का एक संशोधन अंगीकार किया गया, जिसके द्वारा समिति सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गयी। 21 दिसम्बर, 1995 उक्त संशोधन अनुमोदित कर दिया गया।
समिति के सदस्यों का निर्वाचन राज्य पक्षकारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों की सूचि से गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक राज्य पक्षकार अपने राष्ट्रिकों में से एक व्यक्ति का नामांकन कर सकेगा।
राज्य पक्षकारों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से समिति को अपने द्वारा किये गये उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन दिया है जो उसमें मान्य अधिकारों तथा उन अधिकारों के उपभोग पर की गयी प्रगति को प्रभावी बनाएगा। राज्यों की रिपोर्ट में बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रभावित करने वाले कारकों एवं कठिनाइयों का, यदि कोई कारण हो तो सूचित उसको भी सूचित किया जायेगा। रिपोर्ट में सम्बन्धित राज्य में अभिसमय के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पर्याप्त सूचना समिति को उपलब्ध कराने के लिए अन्तर्विष्ट होगी। समिति राज्य पक्षकारों से यह निवेदन कर सकेगी कि कार्यान्वयन से सुसंगत अग्रिम सूचना प्रदान करें। समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक दो वर्षों में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के माध्यम से महासभा को अपने क्रिया-कलापों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समिति महासभा से सिफारिश कर सकती है कि महासचिव से अनुरोध किया जाये कि वह शिशु के अधिकारों के किसी विशिष्ट मामले में अध्ययन करके सलाह दें एवं सिफारिश करे। शिशु के अधिकारों पर अभिसमय शिशुओं या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्तिगत शिकायत के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। शिशु अधिकार अभिसमय केवल सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त किया है।
शिशु अधिकारों पर अभिसमय के वैकल्पिक नयाचार (Optional Protocols to the convention on the Rights of the Child ) — शिशु के अधिकारों पर अभिसमय के दो वैकल्पिक नयाचार 25 मई, 2000 को न्यूयार्क में अंगीकार किये गये जो कि निम्न प्रकार हैं-
(1) सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अन्तर्ग्रस्त होने पर वैकल्पिक नयाचार – नयाचार का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अन्तर्ग्रस्त सशस्त्र संघर्ष होने के मामले में सीमायें। निर्धारित करना था और विशेषकर उनके नियोजन की आयु बढ़ाना था। युद्ध कार्य में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के वास्तविक रूप से अन्तर्ग्रस्त होने पर रोक लगाने हेतु यह वैकल्पिक नयाचार अंगीकार किया गया था। नयाचार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। इसके अनुसार राज्यों का उत्तरदायित्व होगा कि शिशु के अधिकारों पर अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार नियोजन की न्यूनतम आयु में वृद्धि करें।
वैकल्पिक नयाचार के अनुसार राज्यों का उत्तरदायित्व होगा कि वे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा युद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने पर रोक लगाने के लिए सभी यथासम्भव या साक्ष्य उपाय करे। इसके अनुसार राज्य 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के स्वैच्छिक नियोजन के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक कदम उठायेंगे। नयाचार के अनुसार राज्यों का उत्तरदायित्व होगा कि इसके कार्यान्वयन की सूचना शिशु के अधिकारों पर समिति को देंगे।
(2) बच्चों के विक्रय बाल वेश्यावृत्ति एवं चाइल्ड पोरनोग्राफी पर वैकल्पिक नयाचार – बच्चों के विक्रय एवं बाल वेश्यावृत्ति आदि विरुद्ध बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को अपराध घोषित करते हुए शिशु के अधिकारों पर अभिसमय के उपबन्धों का यह नयाचार अनुपूरक है।
नयाचार बच्चों के विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति एवं चाइल्ड पोरनोग्राफी को परिभाषित करता है। यह अपराधियों, पीड़ितों की सुरक्षा एवं निवारण हेतु उपाय सहित उपबन्धों का उल्लंघन करने पर राज्य की विधि का स्तर निर्धारित करता है। यह नयाचार इस सम्बन्ध में, विशेषकर अपराधियों के अभियोजन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराता है ।
प्रश्न 4. महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की संक्षिप्त रूप से समीक्षा कीजिए। Discuss briefly the International Conventions Relating to the Rights of Women.
उत्तर- महिलायें, मानव प्रजाति की एक प्रमुख अंग हैं तथा महिलायें मानव होने के कारण मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतन्त्रताओं को धारण करती हैं। किन्तु महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन समाज के प्रबल वर्ग द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। महिलाओं के अनेक आन्दोलनों ने मानव अधिकारों का संदेश फैलाने में बहुत अधिक योगदान किया है। इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय बनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं-
महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग – सर्वप्रथम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्यधिक भेदभाव रोकने के लिए सन् 1946 में महिलाओं को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ‘महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग की स्थापना की गयी।
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव की अग्राह्यता के सिद्धान्त को अभिपुष्ट कर दिया था और यह उद्घोषणा की थी कि सभी मानव गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतन्त्र एवं समान पैदा हुए हैं अतः इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 7 नवम्बर, 1967 को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय 18 दिसम्बर, 1979 को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। अभिसमय 1981 को प्रवृत्त हुआ और 1 अक्टूबर, 2004 तक इसके 178 राज्य पक्षकार बन चुके हैं।
अभिसमय द्वारा अनुच्छेद के अन्तर्गत ‘महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव शब्द से आशय ऐसा कोई भेद है जिसका प्रभाव महिलाओं द्वारा उनकी वैवाहिक स्थिति पर बिना विचार किये हुये राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल अथवा किसी अन्य क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्री की समानता के आधार पर महिलाओं द्वारा समान स्तर पर उपभोग अथवा प्रयोग करने से वंचित करती है।
अभिसमय ने भाग-3 के अन्तर्गत ऐसे कई क्षेत्रों का प्रतिपादन किया है जहाँ राज्य पक्षकारों के लिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के लिए कहा गया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
1. शिक्षा (Education) अनुच्छेद 10 के अन्तर्गत अभिसमय उपबन्ध करता है कि शैक्षिक पथ-प्रदर्शन में महिलाओं के लिए वैसी ही शर्तें उपबन्धित की जायेंगी जैसी कि पुरुषों के लिए बनाई गयी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार होगा, कोई लिंग भेद नहीं किया जायेगा।
2. नियोजन (Employment) अभिसमय के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान होंगे-
(क) विशेष रूप से काम करने का अधिकार,
(ख) समान नियोजन के अवसर के अधिकार,
(ग) व्यवसाय तथा नियोजन चुनने का स्वतन्त्र अधिकार,
(घ) समान पारिश्रमिक पाने का अधिकार,
(ङ) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
3. स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Care) — अभिसमय का अनुच्छेद 12 यह उपबंध करता है कि राज्य पक्षकार स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की प्राप्ति में जिसमें परिवार नियोजन भी सम्मिलित है, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दर करने की कार्यवाही करेंगे।
4. सामाजिक तथा आर्थिक जीवन (Social and Economic Life) अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करें तथा उन्हें भी वही अधिकार मिले जो पुरुषों को प्राप्त हैं।
5. ग्रामीण महिलायें (Rural Women) अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि ग्रामीण महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करें राज्य पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे ऐसी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करें-
(क) सभी स्तरों पर विकास योजना और उसके अनुपालन में भागीदारी करना।
(ख) पर्याप्त स्वस्थ्य सुरक्षा सुविधा प्राप्त करना तथा परिवार नियोजन की सूचना प्राप्त करना।
(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से सीधे लाभ प्राप्त करना।
(6) विधि के समक्ष समानता (Equality before Law)—अभिसमय का अनुच्छेद 15 यह उपबन्ध करता है कि राज्य पक्षकार विधि के समक्ष पुरुषों के साथ महिलाओं को समानता प्रदान करेंगे। महिलाओं द्वारा की गई संविदा को उनके द्वारा पूर्ण करने और सम्पत्ति का प्रशासन करने में समान अधिकार रखेंगी और राज्य पक्षकार न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में तथा प्रक्रिया की समान अवस्थाओं में उनसे समान व्यवहार करेंगी।
(7) विवाह तथा परिवार सम्बन्ध (Marriage and Family Relationship)— अभिसमय का अनुच्छेद 16 यह उपबन्ध करता है कि राज्य पक्षकार विवाह तथा परिवार सम्बन्धी सभी मामलों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के सभी उपाय करेंगे। अभिसमय के राज्य पक्षकारों ने औरतों के विरुद्ध भेदभाव की इसके सभी रूप में भर्त्सना की है और हर सम्भव साधन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि-
(1) पुरुष एवं महिलाओं की समानता के सिद्धान्त को अपने राष्ट्रीय संविधानों अथवा अन्य उपयुक्त विधायनों में शामिल करेंगे, यदि यह सिद्धान्त उनमें पहले से शामिल न हो
(2) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध करते हुए उपयुक्त विधायी एवं अन्य उपायों को अंगीकार करेंगे;
(3) पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं के अधिकारों के विधिक संरक्षण की स्थापना करेंगे;
(4) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के किसी कार्य अथवा अभ्यास में संलग्न होने से विरत रहेंगे तथा
(5) किसी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभव को समाप्त करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनायेंगे।
अभिसमय के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अभिसमय के प्रावधानों के क्रियान्वयन में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार करने के उद्देश्य से ‘महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर समिति’ (CEDAW) की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया।
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 7 अक्टूबर, 1999 को महिलाओं के विरुद्ध सभी रूपों में भेदभाव की समाप्ति के लिए अभिसमय पर ऐच्छिक नयाचार को अंगीकार किया, जिससे लैंगिक भेदभाव, यौन-शोषण एवं अन्य दुरुपयोग से पीड़ित महिलाओं को तथा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिए नयाचार के राज्य पक्षकारों के विरुद्ध सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार से नयाचार सरकारों को उनकी व्यथाओं के अन्वेषण करने के लिए समिति गठित करने के लिए स्वीकृति देगा। इस प्रकार से वे राज्य जो ऐच्छिक नयाचार के पक्षकार बन जाते हैं, संसूचनाओं को प्राप्त करने एवं उन पर विचार करने के लिए समिति की सक्षमता को मान्यता प्रदान करते हैं। नयाचार के अनुच्छेद 21 के अनुसार नयाचार उस समय लागू होगा जब इसका अनुसमर्थन 10 राज्यों द्वारा हो जायेगा। नयाचार वर्ष 2001 में लागू हो गया। इस समय 67 राज्य इसके पक्षकार बन चुके हैं।
उपर्युक्त अभिसमयों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्यायोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (1976-1985) के दौरान कुल तीन महिला विश्व सम्मेलन आयोजित किये गये। पहला सन् 1975 में मैक्सिको सिटी में, दूसरा सन् 1980 में कोपेनहेगम सम्मेलन तथा तीसरा सन् 1985 में नैरोबी सम्मेलन आयोजित किया गया। चौथा विश्व महिला सम्मेलन सन् 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में सम्पन्न हुआ जो राष्ट्रीय महिला आन्दोलनों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अमूल्य कड़ी का आधार बना। बीजिंग सम्मेलन में कहा गया कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं इसमें महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक एवं निजी जीवन में हिंसा के मामलों को मानव अधिकार का मामला माना जायेगा। बीजिंग सम्मेलन में किसी भी ऐसे संघर्ष की समाप्ति की अपेक्षा की गयी जो महिलाओं के अधिकारों एवं कतिपय परम्परागत या रूढिगत प्रचलन, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों एवं धार्मिक अतिवादिताओं के बीच उत्पन्न होते हैं।
इतना सब होने के बावजूद भी महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्ति के लिए हुए सम्मेलन व अभिसमय अपना वांछित प्रभाव नहीं डाल सके क्योंकि महिलाओं के मानवाधिकारों का विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न तरीकों से उपेक्षा एवं उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई है, जिससे कोई भी देश, कोई भी समाज एवं कोई भी समुदाय मुक्त नहीं है। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय करारों के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होते हैं। अतः हमें आशा ही नहीं दृढ़ संकल्पित होकर ईमानदारी से प्रयास करना होगा तभी महिलाओं की प्रास्थिति बदलेगी, अन्यथा नहीं।
प्रश्न 5. बालक के अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1989 पर समीक्षात्मक चर्चा कीजिए। Critically discuss on the International conventions on the Rights of the Child, 1989.
उत्तर- बालकों को शैशवावस्था में विशेष देखभाल एवं सहायता की आवश्यकता होती। है जिसका उल्लेख मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 के परिच्छेद 2 में किया गया है। कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि बालकों की देखभाल पारिवारिक स्नेह और प्रसन्नता के वातावरण में प्यार एवं समझ से होनी चाहिए। यद्यपि शिशुओं की देखभाल एवं विकास के लिए सिद्धान्त को उद्घोषणा तो की गयी किन्तु ये सिद्धान्त राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थे। अतः यह महसूस किया गया था कि ऐसी अभिसमय तैयार किया जाय जो राज्यों पर विधिक रूप से वाध्यकारी हो। इस कमी को पूरा करने के लिए 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बालकों के अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1989 पारित किया जो 2 सितम्बर, 1990 को लागू हुआ। वर्तमान समय में इस अभिसमय के 192 राज्य पक्षकार बन चुके हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं. और यह तीन खण्डों में विभाजित हैं।
अनुच्छेद के अनुसार, शिशु (बालक) ऐसे प्रत्येक मानव को कहा जायेगा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, यदि शिशुओं पर लागू किसी विधि के अन्तर्गत वयस्कता इससे पूर्व नहीं प्राप्त हो जाती।
बालकों के अधिकार (Rights of the child )—इस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में बालकों को अनेक अधिकार दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं-
(1) प्राण का अधिकार ( अनुच्छेद 6, परिच्छेद 1)।
(2) राष्ट्रीयता अर्जित करने का अधिकार (अनुच्छेद 7)।
(3) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 13, परिच्छेद 1) |
(4) विचार, अन्त:करण एवं धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 14, परिच्छेद 1)
(5) संगम की स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण सभा करने का अधिकार (अनुच्छेद 15 , परिच्छेद 1)।
(6) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 28, परिच्छेद 1 ) ।
(7) सामाजिक सुरक्षा से लाभ का अधिकार (अनुच्छेद 26, परिच्छेद 1)।
(8) शिशु के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास हेतु पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 27, परिच्छेद 1)।
(9) स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर के उपभोग तथा बीमारी के उपचार एवं स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हेतु सुविधाओं का अधिकार ( अनुच्छेद 24, परिच्छेद 1)।
(10) शिशु की एकान्तता, परिवार, गृह या पत्राचार में मनमाना एवं विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप के विरुद्ध विधिक संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 16, परिच्छेद 1)।
शिशुओं (बालकों) के अधिकार पर एक समिति का अभिसमय के अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है जिसमें उच्च नैतिक स्थिति एवं मान्य क्षमता वाले 18 विशेषज्ञ होते हैं। समिति के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा राज्य पक्षकारों द्वारा नामित सदस्यों की सूची से किया जायेगा। प्रत्येक राज्य पक्षकार अपने स्वयं के राष्ट्रिकों के बीच एक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।
राज्य पक्षकारों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से समिति को अपने द्वारा किये गये उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन दिया है जो उसमें मान्य अधिकारों तथा उन अधिकारों के उपभोग पर की गयी प्रगति को प्रभावी बनायेगा। राज्य पक्षकारों से पहली रिपोर्ट अभिसमय लागू होने के दो वर्ष के भीतर तथा बाद में 5 वर्ष में देने की अपेक्षा की जाती है। राज्यों की रिपोर्ट में बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रभावित करने वाले कारकों एवं कठिनाइयों का, यदि कोई हो, का भी संकेत किया जायेगा। लेकिन बालक अधिकार अभिसमय के अन्तर्गत बालकों के द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा समिति के समक्ष व्यक्तिगत परिवाद ले जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बालक अधिकार अभिसमय ने अधिकतर राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त किया है। अभिसमय ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रदान किया है जिसके विरुद्ध राज्यों के व्यवहार की माप की जा सकती है और उसमें सुधार किया जा सकता है। सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के समय से अपनाये गये उल्लेखनीय उपाय हैं-वियतनाम में किशोर न्याय प्रणाली में सुधार, बारबाडोस में अल्पवयों के फाँसी देने का प्रतिषेध तथा नामीबिया के संविधान में अभिसमय के एक भाग को शामिल कया जाना। भारत ने दिसम्बर, 2000 में बालक अधिकार अभिसमय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मामलों को प्रभावी बनाने के लिए और शिशुओं के हितों व कल्याण के संरक्षण के लिए किशोर न्याय (शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित किया है। किशोर न्याय (शिशुओं की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के द्वारा दोनों लिंगों के किशोरों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। भारतीय विधि को अभिसमय से अभिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अनुकल्पों का प्रावधान किया गया है जो किसी शिशु को उसके पुनर्वास, दत्तकग्रहण, पालन सम्बन्धी देखभाल का प्रावधान किया गया है। अनाथ परित्यक्त उपेक्षित एवं शोषित बच्चों के पुनर्वास के लिए पद्धतियों में से किसी एक के प्रायोजित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।
शिशु के अधिकार अन्य संक्राम्य हैं और वह राज्य जो उनके अधिकारों की उपेक्षा करता है, निश्चित रूप से, मानवता की कमी का दोषी है। फिर भी मानव अधिकारों के करोड़ों पीड़ित व्यक्तियों में से बालक भी एक हैं। बालक समाज के सर्वाधिक दुर्बल वर्ग के लोगों में से हैं विशेष रूप से संघर्ष अथवा अन्य आपातकाल की स्थितियों में अतः अभिसमय तभी सफल होगा जब राज्य एवं अन्य संगठन या संस्थायें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करें ताकि बालकों के अधिकारों का संरक्षण व उनकी उचित देखभाल हो सके। अन्त में लेखक का मत है कि कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा राज्यों का अपने-अपने देश के लिए बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाई गयी विधियाँ तभी सार्थक हैं जब इनका उचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाय और संयुक्त राष्ट्र संघ को और मजबूती प्रदान किया जाय ताकि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में उल्लेखित उपबंधों को राज्यों पर बाध्यकारी बनाया जा सके तभी दुर्बल वर्ग जैसे बालक व महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा अन्यथा नहीं।
प्रश्न 6. बच्चों के सन्दर्भ में भारतीय संविधान में दिये गये प्रावधानों पर एक निबन्ध लिखिए। Write an essay on the constitutional provisions relating to special concern of children.
उत्तर- भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में आज भी लड़की का जन्म होना खुशी की बात नहीं समझी जाती। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख स्त्री भ्रूण हत्या होती है। सबसे दुख की बात यह है कि हजारों बच्चियों की हत्या माँ के गर्भ में ही लिंग की जानकारी करके कर दी जाती है। अवैधानिक रूप से गर्भ समापन एवं महिला शिशु हत्या की सूची में आज भारत पूरे विश्व में सबसे ऊपर है।
हमारे संविधान में बालकों के सन्दर्भ में अनेकों प्रावधान किये गये हैं जिनमें बालकों को सुरक्षा, बाल श्रम एवं शिक्षा सम्बन्धी अनेकों प्रावधान सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों को संकटपूर्ण नियोजनों में लगाने का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों (जिसमें बालिकायें भी सम्मिलित हैं) को किसी कारखानें या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वस्तुतः बच्चे देश के भावी नागरिक है; इसलिए संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखें और इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुँचाने वाले पेशे को न अपनाएँ। राज्य द्वारा अपने इस कर्त्तव्य के पालन में बालक नियोजन अधिनियम, 1938 और बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 पारित किया है। बालक नियोजन अधिनियम, 1938 चौदह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रेलवे और अन्य यातायात सम्बन्धी कामों में नियुक्त करने का प्रतिषेध करता है। भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, शिशु अधिनियम, 1961 कारखानों और खानों में 14 वर्ष के बच्चों की नियुक्ति करने का प्रतिषेध करते हैं।
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1983) एस० सी० 1473 के मामले में यह तर्क दिया है कि भवन निर्माण कारखाने में एम्पलायमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, 1939 लागू नहीं होता है, क्योंकि अधिनियम की अनुसूची में “निर्माण कार्य ” का उल्लेख नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि भवन निर्माण कार्य अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत एक जोखिम वाला कार्य है, अतः उसमें 14 वर्ष के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है, भले ही उसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में न किया गया हो। न्यायाधिपति श्री भगवती ने इस बात पर दुःख प्रकट करते हुए राज्य सरकारों को सलाह दिया कि “भवन निर्माण कार्य” को अधिनियम में शामिल करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाएँ और इसको सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 24 के संवैधानिक आदेश का देश के किसी भी भाग में उल्लंघन न किया जाये।
एम० सी० मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, (1996) 6 एस० सी० सी० 756 के अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री मेहता द्वारा लोकहित वाद फाइल करके दक्षिण भारत के शिवकासी में दियासलाई और पटाखा बनाने वाले कारखानों में हजारों की संख्या में कार्य कर रहे बालकों की दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और यह निवेदन किया कि न्यायालय बालकों के कल्याण के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को समुचित निर्देश दे। न्यायालय ने ऐसे बालकों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित किया है-
(1) न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फण्ड की स्थापना किया जाए जिसमें नियोजक प्रति बालक के लिए 20,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा करे, जिसका प्रयोग उनके पुनर्वास के लिए किया जाए।
(2) नियोजक का दायित्व बालकों को कार्य से मुक्त करने के पश्चात् समाप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार को यह निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार के एक वयस्क को कारखाने या अन्यत्र उसके बदले नौकरी दी जाए।
(3) उन मामलों में जहाँ ऐसा वैकल्पिक काम देना सम्भव नहीं है वहाँ समुचित सरकार अपने अंशदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालक के खाते में जहाँ वह कार्यरत है, 5000 रुपये जमा करेगी।
(4) वयस्क काम पाने पर बालक को काम से हटा लेगा। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता है तो भी संरक्षक को यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्त करके बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे और 25,000 रुपये की रकम पर मिले व्याज से बालक की शिक्षा का खर्च 14 वर्ष की आयु तक चलाये।
(5) जहाँ तक खतरे से रहित कारखानों का प्रश्न है, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारें यह देखें कि बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घंटे से अधिक न हो और वे प्रत्येक दिन 2 घण्टे शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा का पूरा व्यय नियोजक वहन करेगा।
न्यायालय का उक्त निर्णय स्वागत योग्य है और इसके फलस्वरूप बालकों की स्थिति में सुधार अवश्यम्भावी है। संविधान में बालकों के शिक्षा सम्बन्धी उपबन्ध अनुच्छेद 45 में किये गये हैं, जिनमें 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 में संशोधन कर यह उपबन्धित किया गया है, कि “राज्य छः वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा।”
अनुच्छेद 45 में उपर्युक्त संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि नए अनुच्छेद 21 (क) द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि “राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बना कर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।”
यूनीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (1993) 1 एस० सी० सी० 645 के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का सांविधानिक दायित्व है। क्योंकि अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। किन्तु उच्च शिक्षा पाने के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।
बाल कल्याण के सम्बन्ध में लक्ष्मी कान्त पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1984) 2 एस० सी० सी० 244 के वाद में एक रिट याचिका एक पत्र के आधार पर दायर की गयी थी जिसके द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने जैसा अनाचार सामाजिक संगठन एवं एजेन्सी द्वारा किया जाता है। यह अभियोग लगाया गया था कि कम आयु के बच्चों को गोद देकर दूर विदेशों में भेज दिया जाता है जहाँ पर उन्हें जीवन का खतरा रहता है और यदि वे जीवित भी रहते हैं तो उन्हें कोई संरक्षण नहीं प्राप्त होता और इस प्रकार वे बाद में भिखारी या वेश्यावृत्ति के कार्य में लग जाते हैं। न्यायमूर्ति भगवती ने अभिनिर्धारित किया कि कुछ सिद्धान्तों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी माता-पिता को बच्चों को गोद दिया जाय या नहीं। बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने सरकार तथा विभिन्न एजेन्सियों को जो कि इस कार्य में लगी थीं, यह निर्देश दिया कि इस प्रकार के मामलों में इन सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाय क्योंकि बालकों का कल्याण सुनिश्चित करना संविधान के अनुच्छेद 15 (3) तथा 39 (ग) तथा (च) के अन्तर्गत यह उनका संवैधानिक दायित्व है।
प्रश्न 7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-
(1) महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग
(2) राष्ट्रीय महिला आयोग,
Write short note on the following-
(1) Commission on the status of women,
(2) National Commission for women
उत्तर (1) – महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग (Commission on the status of women)—महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में की गयी थी। प्रारम्भ में आयोग में 15 सदस्य थे जो 1991 तक बढ़कर 45 हो गये हैं। आयोग वर्ष में दो बार वियना में पूरे विश्व में महिलाओं की समानता के प्रति उन्नति का परीक्षण करने के लिए बैठक करता है। आयोग का प्रमुख कार्य सिफारिशें करना और महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की के लिए रिपोर्ट तैयार करना एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की सिफारिश करना है। आयोग महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से संधियों के प्रारूप तैयार करता है।
आयोग के अनुसार महिलायें किसी क्षेत्र में तब तक उन्नति नहीं कर सकती हैं जब तक वे पुरुषों के साथ निर्णय करने के अधिकार में भाग नहीं लेती। आयोग ने वर्ष 1949 में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों के अभिसमय पर कार्य करना प्रारम्भ किया। अभिसमय जो महिलाओं के अधिकार के सम्बन्ध में प्रथम विधिक लिखित था, महासभा द्वारा वर्ष 1952 में अंगीकार किया गया। आयोग ने वर्ष 1979 में महासभा द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु अभिसमय को अंगीकार करने में भी मदद किया। आयोग ने विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभिसमय को तैयार करने का भी प्रयास किया था, जिसे महासभा द्वारा वर्ष 1957 में अंगीकार किया गया। इसके अतिरिक्त महिला आयोग ने ऐसे बहुत से विषयों पर प्रभाव डाला है जो महिलाओं के विकास, परिवार नियोजन, शिक्षा एवं आर्थिक अधिकारों के क्षेत्र में उनकी भूमिका से जुड़े हुए हैं।
उत्तर (2) – राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for women) – राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम वर्ष 1990 में पारित हुआ था। इस अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी जो अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये कार्यों का सम्पादन करेगा। आयोग अधिनियम की धारा 10 के अनुसार उल्लिखित कार्यों का सम्पादन करेगा। जिनमें से मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-
(i) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों (Safeguards) से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण (Investigation) और परीक्षा (Examine) करना;
(ii) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान (Existing) उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन (Review) करना और उनके यथोचित संशोधनों की सिफारिश करना;
(iii) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं से सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
(iv) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिकायतों (Complaints) की जाँच करना और स्वप्रेरणा (Suo Moto) से ध्यान देना।
(क) महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामले:
(ख) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाली अधिनियमित (Enacted) विधियों के अक्रियान्वयन (Non-implementation) से सम्बन्धित मामले:
(ग) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन (Evaluation) करना, आदि।
परन्तु आयोग कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अक्षम है। वास्तव में कोई भी इसकी बातों को नहीं सुनता। इसके द्वारा की गई सिफारिशों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके द्वारा जारी किये गये सम्मन को गम्भीरता से नहीं लिया जाता। महिला आयोग अपने सम्मन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय के माध्यम से भेज सकता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा सकता है या पोस्टर के रूप में चिपकवा सकता है। परन्तु महिला आयोग शायद ही कभी ऐसा करता है। जब कभी भी कार्य करने के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण के मामले सामने आये हैं तो आयोग ने केवल शुरू में शोर ही मचाया है और ज्यादा कुछ नहीं किया है।
आयोग बिना पोशाक के पुलिस नहीं है। इसके पास मजिस्ट्रेट की विधिक शक्तियाँ भी नहीं हैं। इसके सदस्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसने अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की है। उनका कहना है कि क्योंकि वे सरकार पर निर्भर हैं अतः उनको बहुत कम शक्तियाँ हैं। कोई भी संस्था दूसरे पर निर्भर होते हुए शक्तिशाली नहीं हो सकती।
राजनीतिक नियुक्तियाँ होती रहेंगी लेकिन उनके कार्य आवश्यक रूप से राजनीतिक नहीं हो सकते। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके सदस्यों ने ऐसा कोई उत्साह नहीं दिखाया।
प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें- Write Short note on the following-
(क) शिक्षा का अधिकार (Rights to Education)
(ख) रैगिंग से रक्षा (Protection from Raging)
(ग) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
(घ) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण
उत्तर (क) – शिक्षा का अधिकार (Rights to Education) — शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का महत्व सर्वविदित है किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्त्तव्य संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में भाग IV में रखा था।
अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्त्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निदेश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति निदेशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है। डॉ० अम्बेडकर ने यह कहा था कि निदेशक तत्व एक पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि एक सांविधानिक दायित्व है और उन्हें लागू न करने पर सरकारों को जनता के समक्ष जवाब देना पड़ेगा और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 45 में विहित स्पष्ट रूप से वर्णित नीति निदेशक तत्व के बावजूद भी सरकारों ने इस ओर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया और संविधान लागू होने के दिन से 60 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी भारत के 40% बालक आज भी शिक्षा से वंचित हैं। वैसे संविधान निर्माता यही चाहते थे कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाय। उनकी यह आकांक्षा हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने विफल कर दिया। इसी बीच उच्चतम न्यायालय ने यूनीकृष्णन के मामले में 6 से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। सभी ओर से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने की माँग उठायी जाती रही। इसके फलस्वरूप सरकार ने 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया।
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता है कि “राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बना कर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।”
इसे कार्यान्वित कैसे किया जाय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों की संख्या करोड़ों में है। राज्य के पास वर्तमान विद्यालयों के संचालन के लिए ही धन नहीं है। राज्य अब केवल विद्यालयों को मान्यता दे रही है, वित्तीय सहायता नहीं। अधिकांश माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जहाँ निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का पूर्ण व्यवसायीकरण हो गया है। अधिकांश प्राइवेट क्षेत्र के विद्यालय धन कमाने के कारखाने बन गए हैं। समाज के सम्पन्न लोगों के बच्चे इन्हीं विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं। शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकार हो जाने के कारण एक व्यक्ति इसके लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकता है और न्यायालय सरकार को आदर्श दे सकता है, किन्तु यदि किसी स्थान पर विद्यालय ही नहीं खुले हैं और खुले हैं तो अध्यापक ही नहीं हैं तो शिक्षा का यह मूल अधिकार प्राप्त करना एक दिवास्वप्न ही प्रतीत होता है। केवल शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना देना ही मात्र समस्या का हल नहीं है बल्कि इसमें सरकार के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को भी आगे आना होगा।
उत्तर (ख) – रैगिंग से रक्षा (Protection from Raging) महिलाओं एवं बालकों की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की पीड़ा को दूर करने की दिशा में भी न्यायालयों द्वारा पहल की गई है। रैगिंग से रक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार माना गया है। रैगिंग को रोकने के लिये अब न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों को काफी दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। रैगिंग रोकने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा प्रधानाचार्यों पर अधिरोपित किया गया है। रैगिंग लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने तथा उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने की व्यवस्था की गई है।
सावेन रमेश बनाम वेणी पोया डेन्टल कॉलेज, ए० आई० आर० (2002) कर्नाटक 264 के मामले में तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किसी विद्यार्थी के साथ गाली-गलौज करने तथा अभद्र व्यवहार करने को भी रैगिंग माना है।
उत्तर (ग) – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) — कभी-कभी एक विशेष समुदय की महिलाओं एवं बच्चों के साथ विभेद किया जाता है। यह बड़े दुःख का विषय है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा यहूदी महिलाओं एवं बच्चों के साथ विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा गोद लेने आदि के मामले में समानता नहीं हो सकती क्योंकि वे किसी विशेष समुदाय के हैं। जैसे कि-
(क) हिन्दू विवाह एक संस्कार होने के साथ-साथ एक संविदा भी है जबकि मुस्लिम विवाह में सांस्कारिक लक्षण का कम महत्व है।
(ख) हिन्दू, ईसाई पारसी तथा यहूदी समुदाय में एक विवाह किया जाता है जबकि मुस्लिम पति चार पलियाँ तक रख सकता है। इस प्रकार मुस्लिम पत्नी के साथ विभेद किया जाता है।
(ग) मुस्लिम विधि में पत्नी को इद्दत की अवधि तक भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है। जबकि अन्य व्यक्तिगत विधियों में पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार तब तक होता है जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती या स्वयं भरण-पोषण के योग्य नहीं हो जाती है।
(घ) पति से पुनर्विवाह हेतु मुस्लिम विधि के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी गई है वह मुस्लिम पत्नी के साथ विभेद करती है।
(ङ) हिन्दू व्यक्तिगत विधि में यौवनागम का विकल्प केवल बालिकाओं को है जबकि मुस्लिम विधि में यौवनागम का विकल्प (ख्यार-उल-बुलूग) का अधिकार बालक एवं बालिकाओं दोनों को है। पुरानी ईसाई व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए उपलब्ध आधारों से उसकी स्थिति निम्न हो जाती थी तथा विभेद होता था क्योंकि पति के समान अधिकार उसे नहीं प्राप्त थे।
(च) मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार में पुत्री को मिलने वाली सम्पत्ति पुत्र को मिलने वाली सम्पति को आधी होती है जबकि हिन्दू तथा ईसाई आदि व्यक्तिगत विधियों में पुत्र तथा पुत्री को उत्तराधिकार में समान हिस्सा प्राप्त होता है।
(छ) एक हिन्दू दत्तक ग्रहण कर सकता है जबकि दूसरी व्यक्तिगत विधियों में दत्तक ग्रहण की व्यवस्था नहीं है। अतः दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के साथ विभेद होता है क्योंकि वे दत्तक ग्रहण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
(ज) सम्पति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 के अन्तर्गत ईसाई, पारसी तथा यहूदी महिलाओं पर पूर्ण रोक लगाते हुए सम्पत्ति अन्तरित की जा सकती है कि
वे अपने पति के जीवन काल में उक्त सम्पत्ति अन्तरित नहीं कर सकती। परन्तु इस प्रकार का उपबन्ध दूसरों के लिए नहीं है।
और इस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
26 जनवरी, 1950 को भरतीय संविधान को अंगीकर किया गया, संविधान के लागू हो जाने से भारत एक गणराज्य बन गया है। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार हम एक स्वतन्त्र नागरिक हो गये हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा राज्य का कर्त्तव्य है कि सम्पूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह अनुच्छेद बनाया गया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विधायन, न कि धर्म, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत विधियाँ लागू होती हैं समान सिविल संहिता द्वारा अधिक्रमित की जा सकती हैं। इस प्रकार कोई भी समुदाय समान सिविल संहिता के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता।
श्रीमती सरला मुद्गल, प्रेसीडेन्ट, कल्याणी तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, ए० आई० आर० (1995) एस० सी० 1531 (1539) के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यह स्पष्ट एवं विस्तृत नीति ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक निरन्तर विद्यमान रही तथा भारत क्षेत्र को धर्म के आधार पर अंग्रेजी शासकों ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया था। जिन्होंने विभाजन के बाद भारतवर्ष में रहने को वरीयता दी। वे पूरी तरह से जानते थे कि भारतीय नेतागणों ने दो राज्यों या तीन राज्यों के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं किया और भारतीय गणतन्त्र में केवल एक राज्य ही होना था “भारतीय राज्य” तथा धर्म के आधार पर कोई भी समुदाय एक अलग इकाई नहीं बना रह सकता।
मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, ए० आई० आर० (1985) एस० सी० 945 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक समान सिविल संहिता विभिन्न विधियों में विश्वास रखने वाले मतभेदों को दूर करके राज्य के एकीकरण में सहायता करेगी। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद अनुच्छेद 44 का विधिक आदेश राज्य द्वारा अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आलोचना करते हुए कहा कि कई सरकारें आयीं और गयीं लेकिन सभी भारतीयों के लिए एक व्यक्तिगत विधि बनाने का प्रयास नहीं कर सकीं। हिन्दू विधि का हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताकरण हो चुका है, जिससे कि विभिन्न स्कूलों तथा ग्रन्थों पर आधारित पुरानी हिन्दू विधि के स्थान पर एक एकीकृत संहिता उपलब्ध हो गयी है। जबकि 80% से ज्यादा नागरिकों को संहिताबद्ध व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत लाया जा चुका हो तो सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रस्तावित न करना न्यायोचित नहीं है। सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सम्बन्ध में दुःख प्रकट करते हुए कहा गया कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 प्रभावरहित है। देश के लिए समान सिविल संहिता बनाने के लिए की गई कोई कार्यवाही का साक्ष्य नहीं है माननीय उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के उपबन्धों के अन्तर्गत तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री को भरण-पोषण का आदेश देते हुए कहा कि धारा 125, दण्ड प्रक्रिया संहिता का एक भाग है न कि दीवानी विधि का जो कि विशेष धर्मों के पक्षकारों के अधिकार एवं कर्त्तव्य परिभाषित करता है। भरण-पोषण करने की सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपेक्षा करना तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वयं भरण-पोषण करने के अयोग्य होना ही धारा 125 के लागू होने को सुनिश्चित करता है। ऐसे उपबन्ध सभी धर्म के लोगों पर लागू होते हैं।
संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत घनिष्ठ सम्बन्धियों का भरण-पोषण करने का दायित्व भुखमरी आदि को मिटाने के लिए है। धारा 125 सही मायने में धर्म-निरपेक्ष है।
परन्तु पुरानी धारणा रखने वाले व्यक्तियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया तथा वोट की राजनीति के कारण मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 बना दिया गया जो कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ए० आई० आर० (1985) एस० सी० 985 के निर्णय से मुस्लिम तलाकशुदा महिला को मिलने वाले लाभों से वंचित करता है। यह विधि तलक शुदा मुस्लिम महिला को कोई भी लाभ नहीं देती बल्कि यह कई कारणों से असंवैधानिक है जैसे कि –
(1) यह तलाकशुदा महिलाओं के साथ धर्म के आधार पर विभेद करती है।
(2) संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार स्त्रियों के लिए बनायी गयी विशेष विधि उनके लिए लाभकारी होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ ऐसी विधि किसी विशेष धर्म की स्त्रियों के लिए बनाने की अनुमति नहीं है।
(3) स्त्रियों का सम्मान और सभी की स्थिति की समानता, अवसर की समानता तथा भारतीय संविधान की उद्देशिका को बन्धुता संरक्षित नहीं होती।
(4) यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्योंकि वर्गीकरण किया जाना अयुक्तियुक्त है।
(5) यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) से असंगत है-
समान नागरिक संहिता का निर्माण लोगों की स्वेच्छा से नहीं किया जा सकता। राज्य को इसका निर्माण करना चाहिए जैसे कि हिन्दू संहिता के मामले में किया गया है जिसका हिन्दुओं द्वारा घोर विरोध किया गया था।
संविधान का अनुच्छेद 25 यह आदेश देता है कि स्वतन्त्र रूप से उन्नत करने तथा धर्म का प्रचार करने आदि का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा मौलिक अधिकारों के भाग 3 के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 सम्मिलित है जो नैसर्गिक न्याय, समानता आदि उपलब्ध कराते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धर्म एवं व्यक्तिगत विधि में आवश्यक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 44 सामाजिक सम्बन्धों तथा व्यक्तिगत विधि से धर्म को अलग करता है। विवाह, उत्तराधिकार तथा इसी प्रकार के धर्म निरपेक्ष वाले अन्य समान विषयों को अनुच्छेद 25, 26 तथा 27 के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। हिन्दुओं की व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत विवाह, उत्तराधिकार आदि विषय सांस्कारिक हैं जैसे कि मुस्लिम या ईसाइयों के मामले में है। सिक्खों, बौद्ध तथा जैन के साथ- साथ समुदायों ने नहीं, यद्यपि संविधान सम्पूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का उपबन्ध करता है। समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध मुस्लिम समुदाय द्वारा होता है क्योंकि वे धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर या अल्लाह तथा पैगम्बर के आदेशों के नाम पर व्यक्तिगत विधि में छोटे से भी संशोधन या परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानों बेगम, में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा बनाया गया था।
फिर में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में कई मुस्लिम देशों सहित भारत में भी संशोधन और संहिताकरण किया जा रहा है।
उत्तर (घ ) – पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण- 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये संविधान का 73वाँ संशोधन खासा महत्वपूर्ण संशोधन रहा। इस संशोधन के द्वारा सन् 1992 में संविधान में संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 (एक-तिहाई) स्थान आरक्षित किये गये। इस व्यवस्थ को कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम स्टेंट ऑफ बिहार, ए० आई० आर० (1996) पटना 112 के बाद में चुनौती दी गई, परन्तु पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस चुनौती को नकार दिया गया।
इसी प्रकार का आरक्षण 74वें संशोधन में महिलाओं के लिए सन् 1992 द्वारा नगरपालिकाओं में भी किया गया है।
इस तरह भारत के संविधान में स्त्रियों एवं बालकों के लिए अनेक कल्याणकारी प्रवधान रखे गये हैं।
प्रश्न 9. राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए जो भारतीय बालकों के कल्याण का प्रयत्न करते हैं। Discuss the Directive Principles of State Policy which attempt of Promote the welfare of Indian Children.
उत्तर – भारतीय संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को उपबन्धित किया गया है। इन सिद्धान्तें के अनुसार भारत में विभिन्न सरकारों यानि कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना है। संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में बालकों के लिये कई विशेष व्यवस्थायें को गई हैं, जैसे कि-
(1) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। [अनुच्छेद 39 (ङ) ]
(2) बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये। [अनुच्छेद 39 (च)]
(3) राज्य बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। [ अनुच्छेद 45]
इस प्रकार उपरोक्त नीति-निदेशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कई अभिनव व्यवस्थायें की गयी हैं। न्यायालयों ने भी समय-समय पर इन नीति-निदेशक तत्वों को क्रियान्विति के सार्थक प्रयास किये हैं।
यूनीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, (1993) एस० सी० सी० 645 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
लक्ष्मी कान्त पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1984) 2 एस० सी० सी० 244 के बाद में एक रिट याचिका एक पत्र के आधार पर दायर की गयी थी जिसके द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि भारतीय बच्चों को विदेशी माता-पिता को गोद देने जैसा अनाचार सामाजिक संगठन एवं एजेन्सी द्वारा किया जाता है। यह अभियोग लगाया गया था कि कम आयु के बच्चों को गोद देकर दूर विदेशों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें जीवन का खतरा रहता है और यदि वे जीवित भी रहते हैं तो उन्हें कोई संरक्षण नहीं प्राप्त होता और इस प्रकार वे बाद में भिखारी या वेश्यावृत्ति के कार्य में लग जाते हैं। न्यायमूर्ति भगवती ने अभिनिर्धारित किया कि कुछ सिद्धान्तों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी माता- पिता को बच्चों को गोद दिया जाय या नहीं। बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्होंने सरकार तथा विभिन्न एजेन्सियों को जो कि इस कार्य में लगी थी, यह निर्देश दिया कि इस प्रकार के मामलों में इन सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाय क्योंकि बालकों का कल्याण सुनिश्चित करना संविधान के अनुच्छेद 15 (3) तथा 39 (ग) तथा (च) के अन्तर्गत यह उनका संवैधानिक दायित्व है।
एम० सी० मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ए० आई० आर० (1991) एस० सी० 417 के मामले में यह कहा गया कि बालकों को माचिस कारखाने में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए जो कि प्रत्यक्ष रूप से बनाने के कार्य से सम्बन्धित है। क्योंकि यह बालकों के नियोजन अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत खतरनाक नियोजन है। हालांकि दुर्घटनाओं को बचाने के लिए उन्हें माचिस बनाने के स्थान से दूर पैकिंग के कार्य में लगाया जा सकता है। सभी बालकों का 5000 रुपये का बीमा होना चाहिए तथा एक सेवा शर्त के अनुसार बीमे की किश्त का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाना चाहिए।
शीला बारसे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1986) 3 एस० सी० सी० 596 के मामले में न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि देश के विभिन्न राज्यों की जेल में 18 वर्ष से कम आयु के कैदी बच्चों के बारे में अधिकारियों द्वारा दी गयी सूचना की सत्यता जानने के लिए एक समाज सेवक को उसकी इच्छानुसार 10 हजार रुपये खर्च हेतु भुगतान करें। तथा उसे आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाय। न्यायालय ने निर्देशित किया कि विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किये गये बाल अधिनियमों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाय तथा लोक सभा को चाहिए कि एक केन्द्रीय विधायन पारित किया जाय।
गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० (1990) एस० सी० 292 के बाद में न्यायालय ने वेश्याओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल तथा हॉस्टल उपलब्ध कराने की माँग को निरस्त कर दिया क्योंकि यह बच्चों के हित में नहीं था। अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत लोकहित वाद के द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया था कि सरकार को वेश्याओं के बच्चों के लिए इस प्रकार का प्रबन्ध करने को निर्देशित किया जाये।
विश्व जागृति मिशन बनाम सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट तथा अन्य, (2001) 6 एस० सी० सो० 577 के नवीनतम मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्थाओं में नये बच्चों की होने वाली रैगिंग की बुराई को दूर करने हेतु निर्देश दिया।
अध्याय 2
लिंग विभेद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण
(Constitutional Protection Against Gender Discrimination)
प्रश्न 10. महिलाओं एवं बालकों के लिए कुछ विशेष उपबन्ध बनाये गये हैं जो उन्हें लिंग विभेद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं। वर्णन करें।
उत्तर- महिलायें एवं पुरुष हमारे सृष्टि की दो अनुपम कृतियाँ हैं। महिलाओं एवं पुरुषों को अलग-अलग स्वरूप प्रदान किया गया है यह सही है कि शारीरिक दृष्टि से महिलायें पुरुष से कुछ कमजोर रही हैं। अतीत में देखा जाय तो आर्थिक दृष्टि से भी महिलायें पुरुषों से कमजोर रही हैं तथा वे पुरुष समाज पर आश्रित भी रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी महिलाओं का परिवार और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महिलायें परिवार और समाज में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही हैं। जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है, उस परिवार को स्वर्ग तुल्य माना जाता है।
लेकिन समय के साथ महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया। लोग महिलाओं को तरह-तरह की यातनायें देने लगे। परिवार और समाज में उनकी उपेक्षा होने लगी। यहाँ तक की उनकी बारे में ये कहा जाने लगा कि-
“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।”
पर जैसे-जैसे देश की ओर बढ़ा वैसे-वैसे नारी की स्थिति में सुधार आने लगा। नारी को अब पुनः उनका गौरव प्राप्त होने लगा। उनके संरक्षण के लिये अनेक कानून बनाये गये। संविधान में भी उसे संरक्षण प्रदान किया गया। समाज में भी अब नारी को श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस तरह देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप नारी का स्वरूप भी बदल गया। इस प्रकार नारी अब न केवल पूर्णतया सुरक्षित है अपितु उसे। संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है। संविधान में नारी को पुरुष के समकक्ष ही नहीं अपितु एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है। हमारा संविधान सामाजिक अवधारणा की लोकहित भावनाओं को आत्मसात् किये हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता, अज्ञानता, रोग एवं असमानता का निवारण करना है। संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समता के मूल अधिकार का हनन संविधान के आधारभूत ढाँचे का अतिक्रमण है। [इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० (2000) एस० सी० 498 ] संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष एवं अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि-
(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर – (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानपायें, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
इस प्रकार अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 (1) एवं (2) से यह स्पष्ट होता है कि केवल लिंग के आकार पर उपरोक्त प्रकार का विभेद नहीं किया जायेगा। विधि के समय पुरुष एवं महिलायें समान होंगी तथा उन्हें विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही केवल महिला होने के आधार पर किसी को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जायेगा। इसी प्रकार केवल महिला होने के आधार पर किसी को राज्य निधि पूर्णतः या भागतः पोषित या साधारण जनता के प्रयोग लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जायेगा काठी रनिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० (1952) एस० सी० 123 के मामले में विभेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि-“विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है।” यदि कोई विधि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर असमानता का व्यवहार करती है तो वह शून्य होगी।
संविधान का अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं एवं बालकों के लिये विशेष उपबन्ध किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।” इसे अनुच्छेद 15 (1) एवं (2) का अपवाद भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिये विशेष उपबन्ध कर सकता है। इसके अनुच्छेद 15 के अर्थान्तर्गत विभेद नहीं मानी जायेगा।
इस व्यवस्था का मुख्य आधार महिलाओं एवं बालकों की स्वाभाविक दशा का पुरुषों से भिन्न होना रहा है। महिलाओं एवं बालकों की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दशा हो ऐसी होती है कि उनके लिये विशेष संरक्षण आवश्यक है। फिर जब संविधान बना था तब देश में महिलाओं एवं बालकों की दशा अत्यन्त सोचनीय थी महिलायें न केवल पुरुषों पर आश्रित थीं, अपितु बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज आदि कुरीतियों की शिकार भी थीं। अतः महिलाओं को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना उचित था।
मूलर बनाम ओरेगन, 12 एल० ए० 551 के मामले में अमरीकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि-” अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते हैं। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।”
यही कारण है कि महिलाओं के लिए कई विशेष विधियाँ बनाई गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिये विशेष प्रसूति सहायता का उपबन्ध किया गया है। यह संविधन के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण नहीं है।
दत्तात्रेय बनाम स्टेट, ए० आई० आर० (1953) बम्बई 311 के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि राज्य केवल स्त्रियों के लिये शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है तथा अन्य ऐसी संस्थाओं में उनके लिये स्थान भी आरक्षित कर सकता है।
यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बम्बई, ए० आई० आर० (1954) एस० सी० 321 के मामले में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497 को चुनौती दी गयी थी। धारा 1497 के अन्तर्गत जारता के लिये केवल पुरुष ही दण्डित होता है, स्त्री नहीं। पिटिशनर द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 497 के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करते हैं क्योंकि जारकर्म के लिये केवल पुरुष को ही दण्डित किया जाता है, स्त्री को उत्प्रेरक के रूप में भी दण्डित नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को नकारते हुये कहा कि यह विभेद केवल लिंग के आधार पर ही नहीं है अपितु स्त्री की विशेष स्थिति के कारण है ।
टी० सुधाकर रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, ए० आई० आर० 1994 एस० सी० 544 के मामले में आन्ध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रार द्वार किसी वर्ग विशेष की दो महिलाओं के नामनिर्देशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया। कुछ विनिर्णयों में महिलाओं के लिये किये गये विशेष उपबन्धों को संवैधानिक माना गया है, जैसे-
(i) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 15 के अन्तर्गत समन की तामील प्रतिवादी के नहीं मिलने पर उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकती है, स्त्रियों पर नहीं। स्त्रियों को तामील से मुक्त रखा गया है।
(ii) भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 354 के उपबन्ध विधिमान्य हैं क्योंकि यह स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं।
(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत स्त्रियों का पुरुष से भरण-पोषण पाने का अधिकार विधि-सम्मत है।
इस प्रकार संविधान में बालकों के लिए भी कतिपय विशेष व्यवस्थायें की गई हैं, जैसे-
(क) संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध,
(ख) संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध,
(ग) अनुच्छेद 39 (च) के अन्तर्गत बालकों की शोषण से रक्षा का उपबन्ध आदि
ट्राइबल मिशन बटालेकी बनाम स्टेट ऑफ ए० आई० आर० (2011) एन० ओ० सी० 26 केरल के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। इसमें यह कहा गया है कि-
(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें विभेद किया जायेगा।
इन दोनों ही उपबन्धों से यह स्पष्ट है कि नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में मात्र महिला होने के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। नियुक्ति एवं नियोजन विषयक ऐसी कोई अयुक्तियुक्त शर्त भी अधिरोपित नहीं की जा सकेगी जो किसी को मात्र महिला होने के आधार पर नियोजन अथवा नियुक्ति से वंचित कर दे। इस सम्बन्ध में एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिर्जा, ए० आई० आर० (1981) का एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में एयर इण्डिया के उस नियम की वैधता को चुनौती दी गई थी जिसके अधीन विमान सेवा परिचारिकाओं को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा उनके प्रथम बार गर्भवती हो जाने पर उन्हें सेवानिवृत्त करने का उपबन्ध था। इस नियम को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि यह व्यवस्था पुरुषों पर लागू नहीं होने से अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 का अतिक्रमण करती है। उच्चतम न्यायालय ने इन शर्तों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे विभेदकारी मानते हुए कहा कि पुरुष को 45 वर्ष की आयु में और महिलाओं को 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करना एक मनमानी व्यवस्था है क्योंकि 35 वर्ष की आयु के पश्चात् परिचारिकाओं की सेवा अवधि में वृद्धि करना या न करना प्रबन्ध निदेशक की इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन इसी मामले में उस व्यवस्था को संवैधानिक करार दिया गया जो परिचारिकाओं के सेवा में प्रवेश के 4 वर्षों के भीतर विवाह न करने का उपबन्ध करती थी। न्यायालय ने कहा-यह परिचारिकाओं के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण दोनों दृष्टियों से हितकर है।
वस्तुतः यह व्यवस्था ‘विधि के समक्ष समानता’ के मूल अधिकार पर आधारित है। ‘विधि के समक्ष समानता’ एक गतिशील अवधारणा है। इसका प्रयोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। [नायर सर्विस सोसायटी बनाम स्टेट ऑफ केरल, ए० आई० आर० (2007) एस० सी० 289]
समान कार्य के लिए समान वेतन
इसी सन्दर्भ में महिलाओं के लिये एक और कल्याणकारी व्यवस्था ‘समान कार्य के लिये समान वेतन’ की है। जब से नारी स्वातन्त्र्य की लहर चली है तब से यह धारणा दिन- प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। अब यह प्रायः सुनिश्चित सा हो गया है कि समान कार्य के लिये महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड महिला कल्याण परिषद् बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए० आई० आर० (1992) एस० सी० का एक अच्छा मामला है। इसमें समान कार्य के लिये पुरुष एवं महिला शिक्षकों के वेतन में भिन्नता को चुनौती दी गई थी। समान पद पर समान कार्य करने वाले पुरुष शिक्षकों को महिला शिक्षकों से अधिक वेतन दिया जाता था। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक मानते हुए महिला शिक्षकों को भी पुरुष शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने के आदेश दिये।
नेहरू युवा केन्द्र संगठन बनाम राजेश मोहर शुक्ला, ए० आई० आर० (2007) एस० सी० 2509 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जहाँ समान कार्य हो, वहाँ सीधी भर्ती व प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में विभेद नहीं किया जाना चाहिये।
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 एवं 24 में महिलाओं एवं बालकों के शोषण के विरुद्ध उपचारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव में दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करते हुए कहा गया है कि-
(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के कोई अनुसार दण्डनीय होगा।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
रैगिंग से रक्षा- महिलाओं एवं बालकों की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की पीड़ा को दूर करने की दिशा में भी न्यायालयों द्वारा पहल की गई है। रैगिंग से रक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार माना गया है। रैगिंग को रोकने के लिए लिये अब न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों को काफी दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। रैगिंग रोकने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों पर अधिरोपित किया गया है। रैगिंग लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने तथा उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने की व्यवस्था की गई है। [विश्व जागृति मिशन बनाम गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० 2001, एस० सी० 2793]
स्त्रियों एवं बालकों का अनैतिक, व्यापार मानव दुर्व्यापार का ही एक अंग है। भारत में न केवल बेगार अपितु स्त्रियों एवं बालकों का अनैतिक व्यापार भी धनी एवं सामन्ती लोगों का फैशल रहा है। कोठों एवं कोठियों पर अबोध बालिकाओं एवं देवदासियों का नृत्य और देह- क्रीड़ा एक आम बात रही है। कभी इसे निर्धनता की आड़ में औचित्यपूर्ण माना गया तो कभी धर्म की आड़ में। चोह कारण कुछ भी हो, इसे कदापी नैतिक नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में भी स्त्रियों की निर्धनता एवं विवशता उन्हें देह व्यापार के धन्धे में ढकेल रही है। वेश्यालय, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड आदि नारी देह व्यापार के अड्डे बने हुए हैं। पाँच सितारा होटलों में देह व्यापार एक आम बात मानी जाने लगी है। इन बुराईयों पर रोक लगाने के लिए संसद द्वारा सन् 1956 में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम पारित किया गया है।
नीति-निदेशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबन्ध – महिलाओं एवं बालकों के लिए संविधान के भाग 4 में नीति-निदेशक तत्वों में कई विशेष उपबन्ध किये गये हैं一
1. राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। (अनुच्छेद 39-क)
2. पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो। (अनुच्छेद 39-घ)
3. पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। (अनुच्छेद 39-ङ)
4. बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें और बालार्के और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये। (अनुच्छेद 39-च)
5. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करेगा। (अनुच्छेद 42)
6. राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 44)
7. राज्य बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 45)
इस प्रकार उपरोक्त नीति निदेशक तत्वों में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कई अभिनव व्यवस्थायें की गयी हैं। न्यायालयों ने भी समय-समय पर इस नीति निदेशकतत्वों की क्रियान्विति के सार्थक प्रयास किये हैं।
पी० चेरीबाकया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए० आई० आर० (1994) केरल 27 के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि “शिक्षा का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार में सन्निहित है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करे।”
सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1995) 3 एस० सी० सी० 635 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार से यह अनुशंसा की गयी है कि वह संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाये, जिसमें सभी नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है।
प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जार्ज वर्गीज, ए० आई० आर० (1997) बम्बई 349 के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा भारतीय तलाक अधिकार अधिनियम, 1869 की धारा 10 को अवैध घोषित कर दिय गया है। इसके अन्तर्गत एक ईसाई महिला को पति से तलाक लेने के लिये जारकर्म के साथ-साथ क्रूरता और अभित्यजन साबित करना आवश्यक था। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल व्यवस्था माना। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 10 एक महिला को उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए विवश करती है, जिससे वह घृणा करती है, जिसने उसे त्याग दिया है या उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ऐसा जीवन पशुवत जीवन है।
विक्रमदेव सिंह तोमर बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए० आई० आर० (1988) एस० सी० 1782 के मामले में नारी निकेतन, पटना की दयनीय दशा पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था। याचिका में कहा गया कि नारी निकेतन में महिलायें अमानवीय दशा में रहने के लिये विवश हैं। नारी निकेतन का भवन अत्यन्त पुराना है। वहाँ न तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और न ही अच्छा खाना मिलता है। बिजली-पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए सरकार को नारी निकेतन की दशा सुधारने का निदेश दिया।
मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, (1996) 1 एस० सी० सी० 666 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिये कर्नाटक से बाहर के छात्रों के लिये 60,000/- रुपये के शुल्क को अनुचित ठहराते हुये इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के 60,000/- रुपये देने की स्थिति में नहीं होने पर उसे प्रवेश से वंचित किया जाना उसके शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार का हनन है।
बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, (1996) 1 एस० सी० सी० 490 के मामले में बोधिसत्व गौतम (शिक्षक) ने शुभ्रा चक्रवर्ती (छात्रा) को विवाह का आश्वासन देकर उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किये तथा अन्ततः विवाह करने से इन्कार कर दिया। इस बीच शुभ्रा दो बार गर्भवती भी हो चुकी थी। उच्चतम न्यायालय ने इसे गम्भीरतम मामला मानते हुये विचारण तक बोधिसत्व से शुभ्रा को अन्तरिम प्रतिकर दिलाया। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण मानकर कई दिशा निर्देश जारी किये हैं।
बिशाका बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए० आई० आर० (1997) एस० सी० 3043 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु कई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। यौन उत्पीड़न को परिभाषित भी किया गया है। किसी कामकाजी महिला से शारीरिक सम्बन्ध करने का प्रस्ताव रखना, यौन सम्बन्ध के लिये याचना करना, यौन सम्बन्धी क्रियाकलाप करना, अश्लील साहित्य दिखाना आदि को यौन उत्पीड़न में सम्मिलित माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि जब तक इस दिशा में कोई समुचित विधि नहीं बन जाती है, तब तक –
(i) सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न पर रोक के लिये समुचित नियम बनाये जायें तथा यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की जाये।
(ii) निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू स्थायी आदेशों में भी उक्त व्यवस्था को सम्मिलित किया जाये।
(iii) कामकाजी महिला के यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर नियोजन की ओर से समुचित कार्यवाही हेतु कदम उठाये जायें।
(iv) यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपने स्थानान्तरण का विकल्प दिया जाये तथा आवश्यक होने पर यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति के स्थानान्तरण की व्यवस्था भी की जाये।
इस प्रकार कामकाजी महिलाओं के मनोबल को कायम रखने तथा उनकी गरिमा को बनाये रखने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये अनुच्छेद 51 (क) में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्त्रियों के सम्मान को भी स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 51 (क) (ङ) के अनुसार-भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह “भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है। हमारे देश में स्त्रियाँ कई कुरीतियों एवं कुप्रभाओं की शिकार हैं। जैसे हम “सती प्रथा” को ही लें। भारत और खास तौर से राजस्थान में राजपूत समुदाय में सती प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रथा को रोकने हेतु राजस्थान में “राजस्थान सती (निवारण) अधिनियम, 1987” पारित किया गया है। इसमें सती होने के प्रयत्न, दुष्प्रेरण, गौरवान्वित करने आदि को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया है।
इसी प्रकार की और भी कई प्रथायें हैं जैसे- दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा आदि। संविधान इन सब प्रथाओं के उन्मूलन का आह्वान करता है।
प्रश्न 11. भारत का संविधान राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वर्ण या जन्मस्थान अथवा इसमें से किसी एक के आधार पर विभेद करने से मना करता है। क्या राज्य लिंग के आधार पर नागरिकों में विभेद कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितयों में?
Constitution of India bars the State from discrimination against any citizen of India on grounds of any religion, race, caste, place of birth or any of them, can the State discriminate the citizens on grounds of sex? If yes, under what circumstances?
उत्तर- भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि-
(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर- (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 (1) व (2) से यह स्पष्ट होता है कि केवल लिंग के आधार पर अर्थात् पुरुष अथवा महिला होने के आधार पर उपरोक्त प्रकार का विभेद नहीं किया जायेगा। विधि के समक्ष पुरुष एवं महिलायें समान होंगी तथा उन्हें विधियों का समान संरक्षण प्रास होगा। साथ ही केवल महिला होने के आधार पर किसी को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश से नहीं रोका जायेगा। इसी प्रकार केवल महिला होने के आधार पर किसी को राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जायेगा।
परन्तु राज्य लिंग के आधार पर कुछ कमजोर वर्गों में विभेद कर सकता है जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं एवं बालकों के लिये विशेष उपबन्ध किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ” अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।” इस प्रकार अनुच्छेद 15 (3) अनुच्छेद 15 (1) एवं 15 (2) का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिये विशेष उपबन्ध कर सकता है। इसे अनुच्छेद 15 के अर्थान्तर्गत नहीं माना जायेगा।
इस व्यवस्था का मुख्य आधार महिलाओं एवं बालकों की स्वाभाविक दशा का पुरुषों से भिन्न होना रहा है। महिलाओं एवं बालकों की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दशा ही ऐसी होती है कि उनके लिये विशेष संरक्षण आवश्यक है। फिर जब संविधान बना था तब देश में महिलाओं एवं बालकों की दशा अत्यन्त सोचनीय थी। महिलायें न केवल पुरुषों पर आश्रित थीं, अपितु बाल विवाह, बहु-विवाह, दहेज आदि कुरीतियों की शिकार भी थीं। अतः महिलाओं को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना उचित था।
मूलर बनाम ओरेगन, 12 एल० ए० 551 के मामले में अमरीकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि” अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते हैं। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को को सुरक्षित रखा जा सके।”
यही करण है कि महिलाओं के लिए कई विशेष विधियाँ बनाई गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिये विशेष प्रसूति सहायता का उपबन्ध किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण नहीं है।
यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बम्बई, ए० आई० आर० (1954) एस० सी० 321 के मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 को चुनौती दी गयी थी। धारा 497 के अन्तर्गत जारता के लिये केवल पुरुष ही दण्डित होता है, स्त्री नहीं। पिटिश्नर द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 497 के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करते हैं क्योंकि जारकर्म के लिये केवल पुरुष को ही दण्डित किया जाता है, स्त्री को उत्प्रेरक के रूप में भी दण्डित नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को नकारते हुये कहा कि यह विभेद केवल लिग के आधार पर ही नहीं अपितु स्त्री की विशेष स्थिति के कारण है।
टी० सुधाकर रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, ए० आई० आर० (1994) एस० सी० 544 के मामले में आन्ध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी वर्ग विशेष की दो महिलाओं के नामनिर्देशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित ठहराया गया।
अध्याय 3
आपराधिक विधि के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार एवं उपचार
प्रश्न 12. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। व्याख्या कीजिए।
What protections have been given to the women under the Indian Penal Code? Explain.
उत्तर- भारतीय दण्ड संहिता लिंग के आधार पर सामान्यतः कोई विभेद नहीं करता। यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह संहिता वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिति को देखते हुए दण्ड संहिता ने स्त्री को यौन अपराध से संरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबन्धों का प्राविधान किया है, जो निम्न हैं-
(1) विवाह सम्बन्धी अपराध हर पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उसी स्त्री अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 493 ऐसे व्यक्ति दण्डित करने का नियम प्रस्तुत करती है जो किसी ऐसी स्त्री को जो उसके साथ विवाहित नहीं है, प्रवंचना से वह विधिपूर्वक विश्वास उत्पन्न करता है कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है तथा ऐसे विश्वास के कारण उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन कारित करता है। वह धारा दोनों वर्ग के पुरुषों के सन्दर्भ में लागू होगी। चाहे विवाहित हो अथवा अविवाहित। इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का आपराधिक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जबकि प्रर्वचना के फलस्वरूप पत्नी होने के विश्वास से ऐसी स्त्री उस व्यक्ति से सहवास या मैथुन कारित करने हेतु अपने को समर्पित कर दे। प्रवंचना इस धारा का महत्वपूर्ण तत्व है, यदि प्रवंचना नहीं है तो यह धारा प्रभावित नहीं होगी जहाँ पर स्त्री एवं पुरुष दोनों यह जानते थे कि उनका सम्बन्ध पति एवं पत्नी का नहीं और इसके बाद भी यदि मैथुन करते हैं तो यह धारा प्रभावित नहीं होगी।
इस धारा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
(i) अभियुक्त द्वारा वैध विवाह की विद्यमानता का असत्य विश्वास दिलाया जाना,
(ii) असत्य विश्वास दिलाये गये व्यक्ति के साथ सहवास या मैथुन करना।
इस धारा के अन्तर्गत अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा विधिपूर्ण विवाह होने के बारे में परिवादिनी में मिथ्या विश्वास पैदा करना आवश्यक होता है। मात्र इस कारण कि कोई हिन्दू विवाह हिन्दू विधि में विहित कर्मकाण्ड के अनुसार नहीं किया गया। इस धारा के अधीन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
(2) सपति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना– जो कोई पति गा पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा, जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास में जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
इस धरा की निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं一
(क) यह कि अभियुक्त पूर्ववर्ती अनुक्रम में वैवाहिक सूत्र में बंध गया था।
(ख) ऐसा पूर्ववर्ती अनुक्रम हुआ कि उसका विवाह विधिपूर्ण था।
(ग) व्यक्ति, जिसके साथ वह वैवाहिक सूत्र में बँधा था वह जीवित था।
(घ) द्वितीय पक्षकार के जीवन काल में ही उसने पुनः विवाह किया था।
इस धारा के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जबकि द्वितीय विवाह के समय पूर्व-विवाह विधिक अस्तित्व विद्यमान रहा हो। कोई भी व्यक्ति यदि पूर्व अवैध विवाह के आधार पर पुनर्विवाह करता है तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं करता है।
जहाँ पर कोई विवाहिता हिन्दू स्त्री अपने पति के रहते हुए मुस्लिम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर किसी मुसलमान या ईसाई से पुनर्विवाह करती है ता वह इस धारा के अन्तर्गत द्विविवाह का अपराध करती है। श्रीमती प्रियावाला बनाम सुरेश चन्द्र, ए० आई० आर० 1971 सु० को० 1153 के वाद में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि इस धारा के अन्तर्गत अभियुक्त को द्विविवाह के अपराध के लिए तभी दोषी ठहराया जायेगा, जबकि दूसरा विवाह सभी आवश्यक धार्मिक कृत्यों से जो दोनों पर लागू हों, सम्पन्न किया गया हो, अभियुक्त द्वारा मात्र यह स्वीकार कर लेना कि उसने दूसरे विवाह का अनुबन्ध किया था, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं माना जयेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो उसका यह कार्य पहली पत्नी के पति अत्यन्त अमानवीय तथा क्रूर होगा। साधारणतया ऐसे व्यक्ति यह मानसिक धारणा बनाये रहते हैं कि दूसरे विवाह के स्थापन का तथ्य अत्यन्त मुश्किल से साबित हो पाता है इसलिए वे कानून की गिरफ्त से अपने को बचा लेंगे। अतः ऐसे व्यक्तियों के दण्ड के अधिरोपण में सहानुभूत और उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह-कर्म पूरा कर लेना- जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाह होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। [धारा 496]
धारा 496 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-
(क) अभियुक्त ने बेईमानी अथवा कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म पूरा किया हो,
(ख) उसने इस कर्म को इस बात का युक्तियुक्त ज्ञान रखते हुए पूरा किया हो कि उसके (तद्वारा) वह विधिक रूप से विवाहित नहीं हुआ है।
जारकर्म- जो ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध को कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा, और दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।
धारा 497 जार कर्म करने की दशा में किसी व्यक्ति को दण्डित करने का नियम प्रस्तुत करती है। कोई व्यक्ति जार कर्म करता है यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति ज्ञान एवं विश्वास का यह युक्तियुक्त कारण रखते हुए कि अमूक स्त्री किसी व्यक्ति की विवाहित पत्नी है ऐसी स्त्री के साथ मैथुन करता है तथा यदि उसने ऐसी स्त्री के पति की सम्मति प्राप्त न की हो तथा बलात्कार की कोटि में न आता हो तो उसे जारकर्म कहा जाता है।
इस धारा में निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-
(क) यह कि अभियुक्त ने किसी ऐसी स्त्री के साथ मैथुन किया हो जो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है या जिसके सम्बन्ध में वह ज्ञान एवं विश्वास का यह युक्तियुक्त कारण रखता है कि अमुक स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है।
(ख) उसने ऐसा मैथुन उस स्त्री के पति की सम्पत्ति अथवा मौनानुकूलता के बिना किया हो।
(ग) इस प्रकार का मैथुन बलात्संग की कोटि में नहीं आता हो।
लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1971) क्रि० ला० ज० 1234 के वाद में पति अपने कार्य-व्यापार के शिलशिले में घर से बाहर गया था, उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्त उसके घर आया, जिस पर पति अचानक आ गया। उसने अभियुक्त को पकड़ा तथा दोनों के मध्य काफी झगड़ा हुआ। उक्त मामले में न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि ऐसी दशा में यह उपधारणा की जा सकती है कि पति ने न तो अपनी सम्मति ही दी थी और न मौनानुकूलता की स्वीकृति। इस धारा के अधीन स्त्री की सम्मति अभियुक्त के विचारण में उसके बचाव का आधार नहीं माना जायेगा।
विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना- जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जायेगा, या फुसलाकर ले जायेगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशस से किसी स्त्री को छिपायेगा या निरुद्ध करेगा। वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा। [498] किसी विवाहिता स्त्री को अयुक्त संभोग करने के उद्देश्य तथा आशय से निरुद्ध रखना या उसके प्रयत्न करने पर भी उसे अपने घर न जाने की दशा में अभियुक्त को इस धारा के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।
पति या पति ने नातेदारों द्वारा क्रूरता सम्बन्धी अपराध- जो किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या
(ख) किसी को इस दृष्टि से तंग करना कि उसकी या उसके किसी नातेदार को सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई माँग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहा है। [धारा 498 (क)]
कर्नाटक राज्य बनाम अनिल पुजारी, (2005) क्रि० ला० ज० 2662, के वाद में पत्नी की मृत्यु से पूर्व पत्नी को दूसरी शादी की सम्मति देने के लिए पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था। इस प्रताड़ना के परिणामस्वरूप पत्नी अत्यधिक तनाव में आ गयी और अपने तीन अवयस्क बच्चों को जहर दे दिया और जहर खाकर आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया। अतः मामले के सम्बन्ध में अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-अ के अधीन दोषसिद्धि प्रदान की गयी।
श्रीमती प्रभाती बनाम राजस्थान राज्य, 2005 क्रि० ला० ज० 3352 राजस्थान के वाद में अभिकथन यह था कि उसके पति और सास ने मृतक पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी तथा डॉक्टर द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर यह साबित किया गया था कि वह कथन करने के लिए समर्थ थी। मृत्युकालीन कथन केवल सास को फँसाता था। अतः मामले के सम्बन्ध में मृत्युकालीन कथन के आधार पर सास को प्रदान की गयी दोषसिद्धि उचित थी।
श्रीमती मीरा बनाम रमेश चन्द्र, ए० आई० आर० 2004 राज० 193 के वाद में जहाँ पति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 498-अ और 324 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-अ अधीन दोषमुक्त कर दिया गया था, किन्तु धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था तो ऐसी दशा में मामले के सम्बन्ध में मत व्यक्त किया गया कि पत्नी ने पति द्वारा कारित क्रूरता साबित कर दिया था। अतः इन परिस्थितियों से क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद प्रदान कर दिया गया।
(3) गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में गर्भपात कारित करने- जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाय तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। [धारा 312]
स्पष्टीकरण – जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आती है।
(1) यह कि अभियुक्त ने किसी स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित किया था,
(2) ऐसी स्त्री गर्भवती थी,
(3) इस प्रकार गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं कारित किया गया था।
स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना- जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना चाहे, वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यों द्वारा कारित मृत्यु – जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाये, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाये – और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाये तो वह आजीवन कारावास से या बताये हुए दण्ड से दण्डित किया जायेगा।
(4) लैंगिक अपराध – बलात्संग- जो पुरुष एतस्मिन्पश्चात् अपवादित दशा में सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छः भाँति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष “बलात्संग” करता है यह कहा जाता है-
पहला-उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध,
दूसरा-उस स्त्री की सम्मति के बिना,
तीसरा- उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके साथ वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है,
चौथा- उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित होने का विश्वास करती है,
पाँचवा- उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देते समय वह स्त्री चित्तविकृति अथवा मत्तता अथवा ऐसे पुरुष द्वारा स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से जड़ीमाकारी अथवा अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन कराने के कारण उस बात की, जिसके लिए वह सम्मति देते हैं, प्रकृति और परिणाम समझने में असमर्थ है,
छठाँ- उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।
स्पष्टीकरण – पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 बलात्संग शब्द की परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ निम्न दशाओं में से किन्हीं एक के अन्तर्गत मैथुन करता है तो वह व्यक्ति ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है-
(क) उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध,
(ख) उसकी सम्मति के बिना, या
(ग) ऐसी सम्मति के आधार पर जो स्त्री की मृत्यु या उपहति के खतरे के भय में डालकर प्राप्त की गयी हो, या
(घ) विश्वास के अधीन सम्मति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपना पति समझकर दी गयी सम्मति के आधार पर, या
(ङ) उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है इस धारा के लिये निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-
(1) यह कि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ मैथुन किया हो,
(2) यह मैथुन अधोलिखित परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के अन्तर्गत किया गया हो।
(अ) उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध,
(ब) सम्मति के बिना,
(स) स्त्री को मृत्यु या उपहति के भय में डालकर सम्मति को प्राप्त करने के उपरान्त,
(च) यह कि सम्भोग करने वाला व्यक्ति उसका विवाहित पति है। पत्नी के मन में ऐसा विश्वास उत्पन्न करके ली गयी सम्मति,
(छ) स्त्री की आयु सोलह वर्ष से कम होने की दशा में सम्मति या बिना सम्मति से, पुरुष का लिंग प्रवेशन स्त्री के गुप्त भाग में हुआ हो।
इस धारा के प्रथम खण्ड के अनुसार बलात्कार उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया जाना चाहिए जो कि पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क को तथा अपनी चेतना में है। इस धारा में प्रयुक्त इच्छा शब्द से संभोग की पूर्ववर्ती इच्छा तात्पर्यित है न कि पश्चातवर्ती इच्छा तात्पर्थित है। इस धारा के द्वितीय खण्ड के अनुसार बलात्कार का अपराध तभी गठित होगा जब स्त्री की सम्मति के बिना कोई व्यक्ति उसके साथ मैथुन क्रिया करके सम्भोग करे। इस धारा के तृतीय खण्ड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को मृत्यु या उपहित के भय में डलकर सम्मति प्राप्ति के उपरान्त मैथुन क्रिया करता है तो वह ऐसी दशा में उस स्त्री के साथ बलात्कार करता है। जहाँ पर कोई स्त्री गिरफ्तारी के वारण्ट से भयभीत होकर किसी पुलिस अधिकारी से लैंगिक सम्भोग कराने की सम्मति दे देती है तो उस दशा में इस धारा का तृतीय खण्ड लागू नहीं माना जायेगा। क्योंकि ऐसी अभिप्राप्त सम्मति में मृत्यु या उपहित के भय का अभाव होता है। [अर्जन राम नवराता राम, (1960) क्रि० ला० ज० 849]
बलात्संग के लिए दण्ड- (1) जो कोई उपधारा, (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगा किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया, परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे। सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।
(2) जो कोई-
(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-
(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं बलात्संग करेगा, या
(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपनी अधीनस्थ किसी अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या
(ख) लोक-सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक-सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या
(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जल प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारी वृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण-गृह स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या
(घ) किसी अस्पताल के प्रवन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या
(ङ) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा, या
(च) किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा; या
(छ) सामूहिक बलात्कार करेगा,
वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। मोरमल बनाम राजस्थान राज्य, 2005 क्रि० ला० ज० 2877 के वाद में, इस बात के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य था कि अभियुक्त, ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। घटना स्थल से अण्डरवियर और कन्डोम प्राप्त हुआ था। मृतक के कपड़े पर पाया रक्त समूह अभियुक्त के रक्त समूह से मिलता था। साक्षियों ने इस बात का साक्ष्य दिया था कि उन्होंने घटना स्थल के नजदीक अभियुक्त को देखा था। मृतक के शरीर पर घाव भी पाये गये थे। तथ्य पारिस्थितिक साक्ष्य दर्शित करते थे। अतः मामले के सम्बन्ध में प्रदान की गयी दोषसिद्धि उचित थी।
बहादुर सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, (2005) क्रि० ला० ज० 2865 के बाद में अभियुक्त ने दस वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। अभिलेख के साक्ष्य बलात्कार का किया जाना साबित करते थे। परिस्थितियाँ यह दर्शित करती थी कि उपहत लड़की और उसके पिता का अभियुक्त को फैसाने का कोई हेतु नहीं था। मामले के सम्बन्ध में प्रथम सूचनौ रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब से लिखायी गयी थी। अतः अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित किया गया और सात वर्षों के कठोर कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया। वेद प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2005 क्रि० ला० ज० 2638 के वाद में अभियुक्त एक पुजारी था और उसने एक विवाहित महिला को व्याधि होने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया था। अभियुक्त द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि घटना के समय वह अभियोक्त्री के घर गया था। अभियोक्त्री के कथन पर सम्प्रेषण चिकित्सीय साक्ष्य से किया गया। अभियोक्ति के शरीर पर क्षतियाँ भी पायी गयी थीं जो झगड़े का संकेत करती थी। मामले के सम्बन्ध में अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को प्रदान की गयी दोषसिद्धि उचित थी।
महेश बनाम साजिद और अन्य, 2005 क्रि० ला० ज० 2441 के वाद में उपहत लड़की द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों से मौखिक मृत्युकालीन घोषणा की गयी थी कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और जिसके कारण उसने सल्फास की गोली खा लिया था। किन्तु अन्वेषणकर्ता अधिकारी से उसने अभियुक्तों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी मृत्यु के पूर्व अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी नहीं लिखायी गयी थी और न ही उसके शरीर पर कोई क्षतियाँ ही पायी गयी थीं। साक्षियों के साक्ष्य में भी विरोधाभास था। इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति उचित थी।
पृथक् रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ सम्भोग – जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। [धारा 376 क]
लोक-सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ सम्भोग- जो कोई लोक-सेवक होते हुए, अपनी शासकीय दशा का लाभ उठाकर किसी स्त्री को, जो लोक- सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक को अभिरक्षा में है अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। [धारा 376-ख]
जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, आदि के अधीक्षक द्वारा सम्भोग – जो कोई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर जेल, प्रतिप्रेषण गृह स्थान या संस्था की किसी स्त्री- निवासी को, अपने साथ ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित किया या विलुब्ध करेगा, जो मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ सम्भोग- जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारीवृन्द में होते, हुए अपनी शासकीय दशा लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ, ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मन जन्ना, ए० आई० आर० 2000 सु० को० 2231 के बाद में बलात्कार के बारे में पीड़ित पक्षकार की चिकित्सीय परीक्षा की जानी थी। चिकित्सीय परीक्षा से डॉक्टर द्वारा इस आधार पर इन्कार किया गया था कि पुलिस द्वारा मामला उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मामले के सम्बन्ध में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षा से इन्कार किया जाना उचित नहीं था।
सामूहिक बलात्कार के मामले में शत्रुघ्न बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1993 क्रि० ला० ज० 120, के वाद में यह अभिनिश्चयन दिया गया कि जहाँ पर कुछ दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और वह भी स्पष्ट थी तथा मामले में यह भी दर्शित किया गया कि बलात्कार से पीड़ित लड़की अभियुक्तों में से एक से शादी करने के लिए इच्छुक थी तथा यह भी दर्शित किया गया कि लड़की परिवन्द नहीं करना चाहती थी किन्तु उसने ऐसा अपने माता-पिता के दबाव में किया तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदर है।
मध्य प्रदेश राज्य बनाम दयाल साहू, 2005 क्रि० ला० ज० 4375 के वाद में बलात्कार सम्बन्धी मामले में डॉक्टर, जिसने अभियोक्ति का परिक्षण किया था, पेश नहीं किया गया था और न ही डॉक्टर की रिपोर्ट में पेश की गयी थी। न्यायालय द्वारा मामले के सम्बन्ध में मत व्यक्त किया कि ऐसा न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है यदि अभियोक्ति का साक्ष्यं तथा अन्य साक्ष्य विश्वसनीय हो।
छोटू हरिजन बनाम राज्य, (2005) क्रि० ला० ज० 3926 राज० के वाद में अभियुक्त द्वारा एक अवयस्क बालिका को उसके माता-पिता के कब्जे से बलपूर्वक ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। स्कूल का प्रमाण-पत्र भी यह दर्शित करता था कि घटना के समय अभियोक्ति अवयस्क थी। अभियोक्ति का मौखिक कथन यह साबित करता था कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया था। अतः बलात्कार के अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित थी। मिजोरम राज्य बनाम जोदुहलियाना, (2005) क्रि० ला० ज० 3756 गौ० के बाद में अभियुक्त अपहृत लड़की के परिवार को जानता था तथा वह उसे किसी दूर के स्थान पर ले गया तथा लैंगिक संभोग के लिए उस पर आक्रमण किया। अपहृत लड़की के साक्ष्य का सम्पोषण चिकित्सीय साक्ष्य कराया गया। केवल यह तथ्य कि अभियुक्त के जननांगों पर कोई क्षति चिकित्सीय साक्ष्य से दर्शित नहीं होती थी। अभियुक्त को संदेह का लाभ दिये जाने का आधार नहीं हो सकता। अतः मामले के सम्बन्ध में अभियुक्त को दोसिद्धि उचित थी।
दहेज सम्बन्धी अपराध- जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु जलने अथवा शारीरिक क्षति के कारण कारित की जाती है या उसके शादी के सात वर्ष के अन्तर्गत किन्हीं भी अन्य कारणों से घटित होती है और यह प्रदर्शित किया जाता है कि उसके मृत्यु के ठीक पहले उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया था या उसे उसके पति अथवा उसके किसी रिश्तेदार द्वार कष्ट दिया गया था। या दहेज के मांग के किसी सिलसिले में तो इस प्रकार के मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति अथवा उसका रिश्तेदार उसकी मृत्यु कारित किया हुआ माना जायेगा। वह कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि सात वर्ष से कम का नहीं होगा, परन्तु जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकता है।
भूरा सिंह बनाम राज्य, 1993 क्रि॰ ला० ज० 2636 (इला०) के वाद में पत्नी को उसके सास-ससुर द्वारा कम दहेज लाने के आरोप में प्रताड़ित किया गया। यह घटना पत्नी के ससुराल में ही हुयी थी। मृतक अस्पताल में अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। इन परिस्थितियों में मृतक की धारा 498-अ के अन्तर्गत दोषसिद्धि की गयी क्योंकि उस समय तक धारा 304- ख प्रभावी नहीं हुई थी।
(5) प्रकृति विरुद्ध अपराध – जो किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रियभोग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
(6) लज्जा भंग सम्बन्धी अपराध – जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से था सम्भाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। [धारा 354] कोई ऐसा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया है, उक्त कार्य को इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय बनाया गया है। इस धारा के अन्तर्गत अपराध के गठन में यह महत्वपूर्ण होगा कि उस स्त्री पर किया गया हमला या आपराधिक बल उसकी लज्जा भंग करने के आशय से किया गया था।
जहाँ पर कोई चौदह वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ सड़क पर टहल रही हो तथा कोई व्यक्ति उसके बालों को पकड़ कर उसे खींचने लगे तो ऐसी दशा में इस धारा के अन्तर्गत अपराधपूर्ण माना जायेगा।
(7) व्यपहरण तथा अपहरण सम्बन्धी अपराध – भारत में व्यपहरण-जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, भारत की सीमाओं से परे प्रवहरण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, वह कहा जाता है। [धरा 360]इस धारा के अन्तर्गत उस दशा में अपराध गठित न होगा जबकि प्रवहरित व्यक्ति ने भारत से परे जाने की अपनी सम्मति दे दी हो।
विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण- जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि कोई नारी हो, तो अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
अपहरण- जो कोई किसी व्यक्ति के किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, कहा जाता है।
धारा 362 के अनुसार अपहरण का अपराध तभी गठित होगा जब कि बल एवं प्रवंचना तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान हो।
इस धारा में प्रयुक्त ‘बल’ शब्द का तात्पर्य विवक्षित बल से नहीं अपितु वास्तव में प्रयुक्त किये गये बल से है। अपहरण का अपराध वहाँ गठित नहीं होगा जहाँ पर एक स्त्री अपनी इच्छा से किसी समारोह में जाती है।
किन्तु जहाँ पर कोई लड़की अभियुक्त के साथ जाने को तैयार नहीं तथा अभियुक्त बल प्रयोग द्वारा उसे अपने साथ ले जाता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त अपहरण के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।
इस धारा के निम्न तत्व हैं-
(क) अभियुक्त ने बलपूर्वक विवाध्यता या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरण दिया हो,
(ख) दी जाने वाली ऐसी विवाध्यत या उत्प्रेरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने का हो।
विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना- जो कोई स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए, अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी यह सम्भव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के अशय से या वह विवश, या विलुब्ध की जायेगी, वह सम्भाव्य जानते हुए संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।
जहाँ पर कोई महिला न तो विवाह करने का आशय रखती है न तो लैंगिक सम्भोग का, तब ऐसी दशा में यदि अभियुक्त उसे बलपूर्वक ले जाता है तो वह इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है।
आनन्धन बनाम राज्य, (1995) क्रि० ला० ज० 632 (मद्रास) के वाद में अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 तथा 376 के अन्तर्गत अभियोजित किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे धारा 376 से इस बात पर विमुक्त कर दिया गया था कि वह सम्भोग की अनुमतिदायी पक्षकार थी तथा उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। जहाँ पर अभियोजक अभियुक्त का नाम डायरी पर नहीं चढ़ा था न तो प्रत्यक्षतः गवाह ही यह स्पष्ट करते हों कि उसका नाम पंचनामा में सम्मिलित किया गया है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ अवश्य दिया जायेगा।
वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय को बेचना- जो कोई अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का खरीदना- जो कोई अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाये यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा, या अन्यथ उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, उसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
प्रश्न 13. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है? व्याख्या करें।
What Protections have been given to the women under the Criminal Procedure Code? Explain.
उत्तर- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को प्राप्त संरक्षण – भारतीय दण्ड संहिता के समान ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी स्त्रियों के हित में उपबन्ध किये गये हैं। ये विशेष उपबन्ध समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान करते हैं। ये आरक्षणकारी उपबन्ध भारत में स्त्रियों की विशेष सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुए किये गये हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत स्त्रियों के हित में कुछ प्रमुख उपबन्ध निम्नानुसार हैं।
(1) संहिता के अन्तर्गत उपबन्ध तथा संरक्षण (क) [धारा 46 (4)] के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में स्त्री सूर्यास्त के उपरान्त तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। अपवादस्वरूप जब इसे गिरफ्तार करना आवश्यक हो, तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करके महिला पुलिस अधिकारी उस स्त्री को गिरफ्तार कर सकती है।
(ख) धारा 47 (2) उपबन्ध करती है कि यदि किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को विश्वास का कारण है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति ने किसी घर में प्रवेश किया है या घर में रह रहा है। तो वह घर में प्रवेश कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। परन्तु धारा 47 (2) उपबन्ध करती है कि यदि ऐसा स्थान स्त्री (गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति नहीं) के वास्तविक कब्जे में है, और वह प्रथा के अनुसार लोगों के बीच उपस्थित नहीं है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे घर या स्थान में प्रवेश करने से पूर्व स्त्री को सूचना देगा कि वह उस स्थान से हटने के लिए स्वतन्त्र है या उसे वहाँ से हटने का समुचित अवसर होगा। तदुपरान्त वह ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है।
(ग) धारा 51 (2) उपबन्ध करती है कि जहाँ पुलिस अधिकारी द्वारा स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस स्त्री की तलाशी पुरुष पुलिस द्वारा न करके दूसरी स्त्री द्वारा शिष्टतापूर्वक की जायेगी। यह आदेशात्मक उपबन्ध है।
(घ) धारा 53 (2) के अनुसार यदि कोई स्त्री गिरफ्तार की जती है तथा उसका चिकित्सीय परिक्षण अपराध सम्बन्धी साक्ष्य हेतु आवश्यक है, तो ऐसा परीक्षण केवल एक रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक द्वारा या रजिस्टर्ड महिला चिकित्सक के पर्यवेक्षण (देखरेख) में किया जायेगा। ऐसा परिक्षण तथा साक्ष्य प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 20 (3) जो कि स्वयं अभियोजन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, का उल्लंघन नहीं करता है।
(ङ) धारा 53-ए (1) के अनुसार बलात्संग के अभियुक्त क परिक्षण करने हेतु रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा आवश्यक बल प्रयोग किया जा सकता है। धारा 164-ए के अनुसार बलात्संग की पीड़ित स्त्री का चिकित्सीय परीक्षण, सूचना प्राप्ति के 24 घंटों के अन्दर किया जायेगा।
(2) वयस्क पुरुष सदस्यों पर सम्मन तामील (धारा 64) – संहिता उपबन्ध करती है कि जब सम्मन की तामील सम्बन्धित व्यक्ति पर नहीं की जा सकती है, तो इसकी तामील सम्बन्धित व्यक्ति के साथ रहने वाले परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकती है तथा किसी वयस्क महिला सदस्य पर नहीं की जा सकती है यह प्रतीत होता है कि ऐसे उपबन्ध का आधार यह है कि स्त्रियाँ अधिकतर अशिक्षित होती हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की होने के कारण सामान्यतः लोगों के सामने, विशेषकर अजनबी व्यक्ति के सामने नहीं आती हैं परन्तु यह उचित प्रतीत होता है कि यदि गृहिणी या परिवार की अन्य महिला वयस्क सदस्य शिक्षित (कम से कम स्नातक) है तो सम्मन पढ़कर तथा उसके विषय में उसे समझकर उस पर उस सम्मन की तामील की जा सकती है। इस प्रकार वह महिला सदस्य परिवार के दूसरे पुरुष सदस्यों को सम्मन के सम्बन्ध में बता सकेगी। अतः इस उपबन्ध में संशोधन की आवश्यकता है।
(3) पत्नी तथा बालकों के भरण-पोषण के लिए आदेश [ धारा 125] – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 के अनुसार हर व्यक्ति का अपनी पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता के भरण-पोषण का मौलिक तथा प्राकृतिक कर्तव्य है। उसका यह विधिक उत्तरदायित्व पति, पिता और पुत्र या पुत्री होने के नाते हैं। यदि वह भरण-पोषण करने के लिए सक्षम है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार हिन्दू माता विवाहित पुत्री से भरण- पोषण की मांग कर सकती है। क्योंकि पुत्र तथा पुत्री समान हैं। यह धारा दाम्पत्य अधिकारों के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध न करके केवल भरण-पोषण से ही ग्राम्बन्धित है।
प्रक्रिया- (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकेगी-
(क) जहाँ वह हो, अथवा
(ख) जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती हो, अथवा
(ग) जहाँ उसने अन्तिम बार यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ निवास किया हो।
(2) ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध भरण- पोषण के संदाय के लिए आदेश देने की प्रस्थापना है, अथवा उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभियुक्ति दे दी गयी हो तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जायेगा और उस रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो समन मामलों के लिए विहित है-
परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाये कि ऐसा व्यक्ति उसके विरुद्ध भरण-पोषण संदाय के लिए आदेश देने की प्रस्थापना है। तामील से जान-बूझकर बच रहा है तो मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिट्रेट मामले को एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और ऐसे दिय गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के अन्दर किये गये आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए उनके अन्तर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबन्धन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे, अपास्त किया जा सकेगा।
(3) धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने से न्यायालयों की शक्ति होगी कि वह खर्चों के लिए ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो।
परथा मजूमदार बनाम श्रीमती शर्मिला मजूमदार, (1999) क्रि० ला० ज० 2444 उड़ीसा के वाद में पत्नी द्वारा अवयस्क बच्चे के भरण-पोषण के लिए अन्तरिम भरण-पोषण के लिए दावे किया गया था। मामले के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में पत्नी द्वारा किये गये ऐसे दावे पर विचार किया जा सकता है।
(घ) अन्तरिम भरण-पोषण जीतेन्द्र नाथ सरकार बनाम दालिया सरकार, 2005 क्रि० ला० ज० 3834 कल०, के वाद में यह किया गया कि अन्तरिम भरण-पोषण पक्षकारों की सहमति से दिया जाता है। और याचिकाकर्ता द्वारा इसका भुगतान कुछ निश्चित अवधि तक किया जाता है और भविष्य में किसी समय ऐसे सहमति के आदेश को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है।
जीतेन्द्रनाथ सरकार बनाम दालिया सरकार, (1999) क्रि० ला० ज० 2444 उड़ीसा के वाद में पूर्व में दिये गये अन्तरिम भरण-पोषण के आदेश की वैधता के बारे में कोई भी अब आवेदन और याचिका विरोधी पक्षकार द्वारा इस आदेश पर विचार करने के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी थी। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि पारिवारिक न्यायालय स्वविवेक से पूर्व में निर्णीत की गयी याचिका पर और अन्तिम भरण-पोषण के बढ़ाये जाने के बारे में विचार नहीं कर सकता है जब तक कि याचिकाकर्ता को सुनवायी का अवसर न दिया जाय।
भीरवाराम बनाम गोमा देवी, (1999) क्रि० ला० ज० 1789 (राज०) के वाद में पत्नी अपने माता-पिता के साथ अपने इच्छानुसार पृथक् निवास कर रही थी। पति द्वारा दुर्व्यवहार का कोई साक्ष्य नहीं था। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पत्नी को भरण-पोषण बिना किसी विश्वसनीय कारण के दिया गया था, किन्तु वह अपने दो बच्चों के लिए भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार थी।
रशीद नाजकी एलियांस बनाम शाहिन गुलाब, (2005) क्रि० ला० ज० 4290, के वाद में पति द्वारा मामले के सम्बन्ध में यह अभिवाक् किया गया कि उसने पत्नी को तलाक दे दिया गया है। इस बात को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई भी तथ्य मौजूद नहीं थे। अतः ऐसी दशा में पत्नी अन्तरिम भरण-पोषण की हकदार थी।
रूपसी एलियांस रूप सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (1999) क्रि० लॉ ज० 1739 (राज०) के बाद में पत्नी का विवाह नारा प्रथा के अनुसार हुआ था। विवाह में आवश्यक वैवाहिक रिवाजों का पालन किया गया था। पक्षकारों में नारा विवाह प्रथा अनुज्ञेय थी। विवाह के पक्षकार 17 वर्षों से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। पक्षकारों के बीच विवाह का होना स्थापित किया गया था, मामले के सम्बन्ध में न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार था।
(ङ) अतिरिक्त भरण-पोषण- श्रीमती जुबेदावी बनाम नियाज मोहम्मद गुलाम मोहम्मद, 1999 क्रि० लॉ ज० 1326 कर्नाटक के वाद में याचिकाकर्ता ने अपने एक पुत्र जो कि तकनीकी सेवा द्वारा धन कमाता था, से भरण-पोषण प्राप्त करने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने अपने दो पुत्रों जो कि कुली का कार्य करते थे के साथ रहती थी उसका भरण- पोषण करने में सक्षम नहीं थे, याचिकाकर्ता तनावपूर्ण दशा में रह रही थी। अतः उसे 300 रुपये का अतिरिक्त भरण-पोषण उस पुत्र जो कि तकनीकी सेवा करता था से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
(च) माँग से अधिक भरण-पोषण-कदार मियां बनाम श्रीमती जेहरा खातून, (1999) क्रि० लॉ ज० 1446 उड़ीसा के वाद में माँग से अधिक भरण-पोषण प्रदान किया गया था। उच्च दर भरण-पोषण दिये जाने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था, न्यायालय ने भरण-पोषण की रकम मांग किये गये भरण-पोषण तक कम कर दिया। इस धारा के अन्तर्गत अधर्मज संतान भी अपने अधिकार के रूप में अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त कर सकता है। इस धारा के अधीन जब कोई अधर्मज सन्तान अपने पिता के विरुद्ध भरण-पोषण हेतु याचिका न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो न्यायालय उचित परीक्षा के पश्चात् उसे भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश पारित कर सकता है। इन याचिकाओं के सन्दर्भ में न्यायालय ऐसी अधर्मज संतान को अंतरिम भरण-पोषण भी दिये जाने के लिए न्यायालय अधिकृत है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तथा धारा 482 के उपबंधों को सम्मिलित रूप से अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि यदि फेमिली न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण हेतु आवेदन अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप निस्तरण कर दिया जाता है तो इसे पुनर्स्थापित करने के लिए फेमिली न्यायालय के पास कोई अन्तर्निहित शक्ति नहीं है। किन्तु यह ऐसा पुनर्स्थापना विवक्षित शक्ति के अध्यधीन किया जा सकता है। पुलिपुल्ला चलिल नारायन कुरूप बनाम थममुल्ला परमवर्थ बलसला, 2005 क्रि० लॉ ज० 3266 केरल में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण के लिए दिया गया पूर्ववर्ती आवेदन संहिता की धारा 125 के अधीन पश्चात्वर्ती आवेदन दिये जाने के लिए वर्जन नहीं है। जहाँ की पत्नी द्वारा भरण-पोषण के लिए पूर्ववर्ती आवेदन पति द्वारा क्रूरता तथा किसी अन्य स्त्री के साथ सम्बन्ध होने के आधार पर दिया गया था किन्तु इन बातों के साबित न होने के कारण खरिज कर दिया गया था तो पत्नी द्वारा गया पश्चात्वर्ती आवेदन पूर्ववर्ती आवेदन के खारिज किये जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा।
गोरखनाथ खाण्डू वेगल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 क्रि० लॉ ज० 3158 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट 1 माह से अधिक का कारावास देने की अधिकरिता भरण-पोषण के प्रत्येक आदेश के उल्लंघन के लिए रखता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) का परन्तुक भरण-पोषण के आदेश की तिथि से 12 माह के भीतर देय रकम की वसूली करने के लिए आवेदन करने का वर्णन करता है। अतः 12 माह की रकम की वसूली एक आवेदन द्वारा की जा सकती है और मजिस्ट्रेट अधिकतम 12 माह का कारावास प्रदान कर सकेगा।
कमलदीप कौर बनाम बलविन्दर सिंह, 2005 क्रि० लॉ ज० 4164 के वाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा भरण-पोषण प्रदान किये जाने की अधिकारिता के सम्बन्ध में अभिमंत व्यक्त किया गया कि मजिस्ट्रेट दावाकृत भरण-पोषण की रकम से भिन्न प्रतिकर की रकम प्रदान करने से वर्जित नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी सभी पर लागू होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यह दुःख का विषय है कि यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 44 यह उपबन्ध करता है कि राज्य सम्पूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। परन्तु समान नागरिक संहिता बनाने के लिए किये गये प्रयास का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। समान सिविल संहिता विभिन्न विधियों में विश्वास रखने वाले मतभेदों को दूर करके राज्य के एकीकरण में सहायता करेगी। यद्यपि विभिन्न धारणाओं वाले व्यक्तियों को एक स्थान (प्लेफार्म) पर लाने में कठिनाइयाँ हैं, परन्तु शुरुआत तो की जानी चाहिए। यदि भारतीय संविधान के कोई मायने है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम महिला (विवाह- विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 मुस्लिम को विशेषाधिकार देने हेतु पारित किया गया है।
(4) उपस्थिति से छूट- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 (1) के अनुसार अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की आवश्यकतानुसार किसी स्थान या थाने पर साक्षी को उपस्थित होना होता है। परन्तु उसके खण्ड (2) के अनुसार स्त्रियों तथा 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष बालकों को इससे छूट होती है। इस प्रकार स्त्रियों तथा 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को साक्षी के रूप में थाने पर आने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त करने हेतु स्वयं उसके निवास स्थान पर जाना होता है।
(5) स्त्री की मृत्यु होने पर शव परीक्षण- आपराधिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के द्वारा संहिता में धारा 174 की एक उपधारा प्रस्तुत की गयी है। यह संशोधन इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि दहेज मृत्यु या विवाहित स्त्रियों के साथ क्रूरता के मामलों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। इस उपबन्ध के अनुसार यदि कोई स्त्री विवाह के सात वर्ष के अन्दर आत्महत्या कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तथा ऐसा सन्देह होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने यह अपराध किया है तो उस स्त्री के किसी सम्बन्धी द्वारा प्रार्थना करने पर शव परीक्षण अवश्य किया जायेगा।
1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा संहिता की धारा 198-ए भी जोड़ी गयी है। उस धारा के अनुसार 498-ए के अन्तर्गत अपराध का विचारण न्यायालय तब तक नहीं करेगा जब तक कि पीड़ित पक्षकार द्वारा यह उसके माता-पिता, भाई-बहन या उसके पिता मातो के भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा सम्बन्धी हो, के द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना शिकायत न की गयी हो, अतः यह उपबन्ध अभियोजन के क्षेत्र का विस्तार करता है तथा पत्नी का कोई भी सम्बन्धी इस सम्बन्ध में शिकायत कर सकता है।
(6) विचारण का स्थान- संहिता की धारा 181 (2) के अनुसार व्यपहरण तथा अपहरण के अपराध की जाँच का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार में व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया था या उस व्यक्ति को छिपाया या निरुद्ध किया गया था। जबकि अन्य मामलों में सामान्य नियम यह है कि किसी अभियुक्त का विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसके क्षेत्राधिकार में अभियुक्त पाया जाता है। अतः स्त्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह उपबन्ध किया गया है।
(7) सदाचरण की परिवीक्षा पर स्त्री को छोड़ना- संहिता की धारा 360 बीस वर्ष से कम आयु के अभियुक्त या किसी भी आयु की स्त्री को विशेष संरक्षण प्रदान करती है। यदि उसने मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध नहीं किया है। यदि अपराधी के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध सिद्ध नहीं होता है तो सदाचरण की परिवीक्षा पर तथा शान्ति बनाये रखने हेतु बाण्ड लिखने पर स्त्री को छोड़ने का आदेश न्यायालय दे सकता है। धारा 360 के अनुसार बाण्ड और छोड़ते समय न्यायालय को अपराधी का पूर्ववृत्त ध्यान में रखना चाहिए। अतः यह धारा लाभकारी है तथा अपराधी पर केवल प्रथम बार लागू होती है। यदि अपराध गम्भीर प्रकृति का नहीं है तो न्यायालय द्वारा धारा के अन्तर्गत इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। संहिता की धारा 361 उपबन्ध करती है कि धारा 360 के अन्तर्गत. शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा ऐसा करने हेतु विशेष कारण उल्लेख करना चाहिए।
(8) गर्भवती स्त्री के मृत्यु दण्ड का विलम्बन- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 415 के अनुसार उच्च न्यायालय अपराधी स्त्री के मृत्यु दण्ड के क्रियान्वयन को विलम्बित कर सकता है, यदि गर्भवती है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त धारा 415 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ऐसा परिवर्तन दण्ड का पुनावलोकन करने पर निर्णय पारित करने के उपरान्त भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।
(9) गैर-जमानतीय अपराधों में स्त्री अपराधी की जमानत- सामान्यतः न्यायालय या पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अन्तर्गत गैर-जमानतीय अपराध के मामले में किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की शक्ति प्राप्त है परन्तु मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध में जमानत पर नहीं छोड़ेगा। यह धारा इस नियम के अपवाद का उल्लेख करती है। इस धारा के अनुसार मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध में भी स्त्री को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
उपर्युक्त सभी प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के अन्तर्गत स्त्री के हित में बनाये गये हैं तथा वे अनुच्छेद 14 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। न्यायालय द्वारा इन प्राविधानों का समय-समय पर परीक्षण किया गया है तथा संविधान बताया गया।