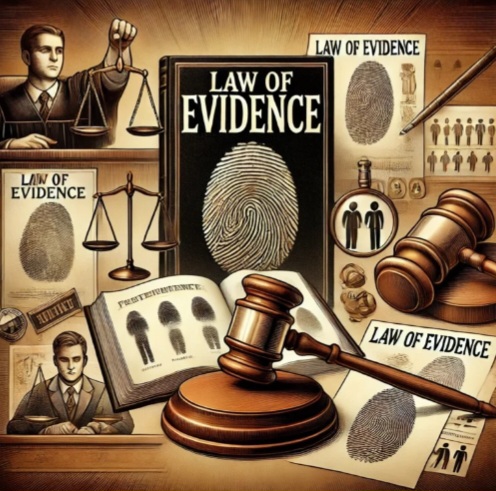-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
प्रश्न. (क) व्याधिक कार्यवाहियों से आप क्या समझते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुछ कार्यवाहियों पर नहीं लागू होता। स्पष्ट करें। What do you understand by Judicial Proceedings? Indian Evidence Act is not applies to some proceeding explain.
(ख) ‘साक्ष्य’ शब्द की परिभाषा दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित विभिन्न साक्ष्यों को बतलाइये। Define “Evidence”. Explain the different kinds of evidence recognised under Indian Evidence Act.
उत्तर (क) – न्यायिक कार्यवाहियाँ (Judicial Proceedings) – भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी न्यायालय के समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। साक्ष्य विधि उन कार्यवाहियों में नहीं होता जो न्यायिक नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 (झ) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में वह कार्यवाही सम्मिलित हैं जिसके दौरान साक्ष्य शपथ पर या तो लिया जाता है या लिया जा सकता है। यह अधिनियम के अधीन सेना न्यायालयों को छोड़कर, अन्य सेवा न्यायालयों पर भी लागू होता है। यह (1) शपथपत्रों पर (ii) किसी मध्यस्थ के सामने की कार्यवाहियों पर और (iii) आर्मी एक्ट के अधीन किसी सैनिक न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों पर नहीं लागू होता अर्थात् कोर्ट मार्शल पर नहीं लागू होता
न्यायालय के दो प्रकार के कर्तव्य हैं। (i) न्यायिक, (ii) प्रशासनिक, ये दोनों एक दूसरे से पृथक एवं भिन्न हैं और उन दोनों में न्यायिक बुद्धि का लगाना आवश्यक है। जैसा कि न्यायाधीश लोटस ने कहा है कि “न्यायाधीश न्यायिक तथा न्याय प्रशासन में कार्य करते हैं और वे न्यायिक रूप से तभी कार्य करते हैं जब कि अपने प्राइवेट कमरे में प्रशासनिक मामले में सही बात का निर्णय देते हैं। साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होता है। यह न्यायिकेतर कार्यवाहियों में नहीं लागू होता लेकिन तथ्य के मामलों में ऐसी जाँच जिसमें किसी विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है और कोई फैसला नहीं दिया जाना होता बल्कि एक निश्चित अवस्था में कोई चीज कर्तव्य के रूप में की जाती है, न्यायिक जाँच नहीं होती, बल्कि ‘प्रशासनिक जाँच’ होती है। न्यायिक कार्यवाही एक विस्तृत शब्द है जिसमें जाँच और परिक्षण दोनों सम्मिलित हैं। जाँच न्यायिक होती है, यदि उसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच या व्यक्ति और सामान्य समुदाय के बीच, न्यायिक सम्बन्ध निश्चित करना है।” यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यहाँ तक कि कोई न्यायाधीश भी यदि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्यवाही नहीं करता है, तो उसकी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही’ नहीं कही जायेगी। न्यायालयों को दो कर्तव्यों अर्थात् न्यायिक तथा प्रशासनिक का निर्वहन करना होता है। वे कर्त्तव्य एक-दूसरे से नितान्त पृथक और भिन्न हैं और उन दोनों में न्यायिक बुद्धि का लगाना आवश्यक है। ८० प्र० स० को धारा 164 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा नियन्त्रित नहीं होता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित को न्यायिक कार्यवाही माना गया है।
(i) किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियाँ।
(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण-पोषण की कार्यवाहियाँ।
(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 97, 145 और 340 के अधीन जाँच।
(iv) औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियाँ
(v) किसी अभिकचन की सत्यता के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच को, जो अधिकरण डिप्टी कमिश्नर को पेश की गई याचिका में अन्तर्विष्ट है।
(vi) साक्ष्य अधिनियम चुनाव याचिका के विवरण में लागू होता है। अवमान की कार्यवाहियों में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है।
न्यायिकेतर कार्यवाहियाँ – किन्हीं तथ्यों के विषय में की गई जाँच जहाँ पर कोई 1 विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता और कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता किन्तु एक कर्तव्य के रूप में निश्चित परिस्थितियों में कुछ करना है तो वह न्यायिक जाँच नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यवाही है इसी प्रकार दण्डाधिकारी के समक्ष की वे कार्यवाहियाँ नहीं है और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन कार्यवाहियों में नहीं लागू होगा।
विभागीय कार्यवाहियाँ (Departmental Proceeding) — विभागीय जाँच उस वर्ग में नहीं आती है जिसमें आपराधिक एवं सिविल कार्यवाहियाँ आती है। अतएव भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबन्ध इन विभागीय जाँचों में नहीं लागू होते हैं तथापि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त उक्त विभागीय जांचों में भी लागू होंगे।
शपथ-पत्र (Affidavits) – भारतीय साक्ष्य अधिनियम शपथ-पत्रों पर लागू नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत शपथ-पत्र साक्ष्य नहीं है जब तक कि वह आदेश 19 सी० पी० सी० द्वारा अनुज्ञात न हो। सपथ-पत्र अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य को परिभाषा के अन्तर्गत नहीं शामिल है और साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग केवल तभी हो सकता है यदि पर्याप्त आधारों पर न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 1 या 2 के अधीन आदेश पारित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता न्यायालय को किसी तथ्य को शपथ-पत्र द्वारा साबित किये जाने का आदेश देने का अधिकार देती है। जब एक पक्षकार शपथ-पत्र दाखिल करता है तो विपक्षी प्रति शपथपत्र दाखिल कर सकता है या वह प्रतिपरीक्षा के लिए राज्यकर्ता की उपस्थिति की माँग कर सकता है। यदि वह इन दोनों में कोई कार्य नहीं करता है तो शपथपत्र के विरुद्ध पूर्णरूप से साक्ष्य हो जाता है यदि इसके विपरीत शपथकर्ता विपक्षी की माँग पर अपने को प्रतिपरीक्षा हेतु हाजिर नहीं करता है तो शपथ-पत्र का सात्यिक मूल्य समाप्त हो जाता है।
मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियाँ- किसी मध्यस्थ के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियों पर यह अधिनियम नहीं लागू होता है। जिसका कारण यह है कि किसी मुकदमे को मध्यस्थ के सुपुर्द करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मुकदमा संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपट जाये और उसमें नियमित बाद जैसी लम्बी-चौड़ी कार्यवाही न करनी पड़े। माध्यस्थम् नियमित न्यायालय नहीं होती और न हम उसे अधिकरण ही कह सकते हैं। इसी कारण माध्यस्थम् की कार्यवाहियों में साक्ष्य सम्बन्धी नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता है। इससे यह न समझना चाहिए कि साक्ष्य के विषय में पंच मनमानी कर सकता है। सच तो यह है यद्यपि वह साक्ष्य के तकनीकी सिद्धान्तों का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता फिर भी वह नैसर्गिक न्याय को तिलांजलि नहीं दे सकता, उसे उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। मध्यस्थ नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।
कमीशन – व्यवहार प्रक्रिया संहिता या दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त किये गये कमिश्नरों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं ऐसा कमिश्नर साक्षियों को बुला सकता है और उनका साक्ष्य लेखबद्ध कर सकता है ताकि यदि वह आवश्यक समझे तो इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर अपना प्रतिवेदन (Report) कर सके।
उत्तर (ख ) – साक्ष्य (Evidence ) – साक्ष्य शब्द से विधिक अर्थों में वे सभी विभिन्न विधिक, साधन सम्मिलित हैं जो जाँच के लिए प्रस्तुत तथ्य को साबित करने के आशय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। दूसरे अर्थों में साक्ष्य की परिभाषा में वे सभी वस्तुएँ आती हैं जिनका झुकाव या उद्देश्य किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में उपधारणा या अनुमान उत्पन्न करना है। परन्तु शपथ पत्र को साक्ष्य की परिभाषा में नहीं सम्मिलित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार- ‘साक्ष्य’ शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-
(1) वे सभी कथन जिनके, जाँचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है; ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सय दस्तावेजें, जिनमें इलेक्ट्रानिक अभिलेख शामिल हैं। ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।
साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य सामग्री भी सम्मिलित है जो किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में न्यायालय के मस्तिष्क में अनुमान उत्पन्न करता है। साक्ष्य शब्द में उन व्यक्तियों का वर्णन सम्मिलित है। जिन्होंने स्वयं किसी तथ्य को होते हुए देखा हो, जैसे कि विस्फोट की आवाज सुनी हो या उसकी चमक देखी हो। हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए० आई० आर० (2014) एस० सी० 1400 के वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यह परिभाषा अपने आप में सम्पूर्ण है। जब भी शब्द “इससे अभिप्रेत है तथा इसमें आते हैं” प्रयोग किए जाते हैं तो एक प्रकार से यह इंगित करता है कि यह पक्के प्रकार की परिभाषा है इसके अतिरिक्त उन शब्दों की कोई भी अन्य परिभाषा नहीं दी जा सकती।
किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों को उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का नाम दिया गया है-
(1) मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य (Oral and Documentary Evidence)
(2) प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Direct and Circumstantial Evidence)
(3) प्रत्यक्ष तथा अनुश्रुत साक्ष्य (Direct and Hearsay Evidence)
(1) मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य (Oral and Documentary Evidence)- किसी बाद या कार्यवाही में एक पक्षकार अपने साथियों को बुलाकर न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य के बारे में साक्ष्य निरूपित करवाता है। साक्षी के ये मौखिक कथन, मौखिक साय कहे जाते हैं। मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होने चाहिए अर्थात् जिस व्यक्ति ने तथ्य को घटित होते हुए प्रत्यक्ष (स्वयं) देखा या सुना हो या अनुभव किया हो, उसी व्यक्ति क न्यायालय में उपस्थित होकर तथ्य के बारे में बताना होगा। मौखिक कथन तब तक साक्ष्य नहीं माना जाता है जब तक कथनकर्ता का (जिरह) प्रति परीक्षण न कर लिया गया हो।
जब एक पक्षकार किसी वाद या कार्यवाही में अपने समर्थन में किसी दस्तावेज (प्रलेख या लेख) प्रस्तुत करता है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। दस्तावेज तभी साक्ष्य बनता है। जब वह न्यायालय के समक्ष जाँच के लिए प्रस्तुत या पेश किया जाता है। दस्तावेज की अन्तर्वस्तु (दस्तावेज की विषयवस्तु) को साबित करने हेतु दस्तावेज ही सर्वोत्तम साध्य है जिसे प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज को उसकी प्रतिषे के माध्यम से (Secondary Evidence) साबित किया जा सकता है जैसे दस्तावेज अचल (दीवाल) या भारी वस्तु हो, दस्तावेज खो गया हो, दस्तावेज नष्ट हो गया हो आदि।
(2) परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) – परिस्थितिजन्य साक्ष्य उन परिस्थितियों का साक्ष्य है जिसमें विवाद्यक तथ्य या मुख्य तथ्य घटित हुआ हो। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि विवाद्यक तथ्य के साथ उनका सम्बन्ध, कारण तथा परिणाम (Cause and Effect) का होता है और उनसे सन्तोषजनक परिणाम पर पहुँचा जा सकता है।
जैसे यदि कही पर पद चिह्न पाये जाते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि जीवित प्राणी उधर से गुजरा होगा। पदचिह्नों से यह भी अन्दाज (अनुमान) लगता है कि गुजरने वाला प्राणी पशु है या पक्षी है या अन्य कोई मनुष्य ।
अभियोजन को परिस्थितियों के मध्य सम्पूर्ण सम्बन्ध दिखाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना हो। अरुण भक्ता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए० आई० आर० (2009) एस० सी० 1225 के बाद में अभियोजन का यह कथन कि पूर्व रात्रि के दौरान अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में था। परन्तु परिवार के सदस्यों का कुछ और ही कहना था।
अतः सभी परिस्थितियों का अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत होना जरूरी है। [मो० आजाद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए० आई० आर० (2009) एस० सी० 1307]
(3) अनुश्रुत साक्ष्य – अनुश्रुत साक्ष्य सुनी बातों के साक्ष्य को कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति, जो न्यायालय में साक्ष्य दे रहा है, तथ्य को घटित होते स्वयं नहीं देखता है तो वह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ज्ञात हुए तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे सकता। सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य को विधि की नजर में कोई साक्ष्य नहीं माना जाता क्योंकि सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य का श्रोता साक्षी न होकर अन्य कोई व्यक्ति होता है तथा सबूत देने वाला व्यक्ति सबूत की सत्यत का उत्तरदायित्व नहीं लेता। इसके अतिरिक्त मूल साक्ष्य को किसी अन्य व्यक्ति ने देखा होता है इसलिए उसके द्वारा कही हुई बातों को साक्षी बढ़ा-चढ़ा कर कह सकता है। परन्तु कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ हैं जहाँ सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपवाद के रूप में सुनी- ‘सुनाई बातों के साक्ष्य के ग्रहण करने की अनुमति है जैसे-मृत्युकालिक बयान, रेस गेस्टा स्वीकृतियाँ तथा संस्वीकृतियाँ आदि।
प्रश्न 2. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये या निम्न को परिभाषित करें-
(1) तथ्य
(2) सुसंगत तथ्य
(3) साबित
(4) नासाबित
(5) साबित नहीं हुआ
Write short notes on the following or define the following-
(I) Fact
(2) Relevant fact
(3) Proved
(4) Disproved
(5) Not Proved
उत्तर – ( 1 ) तथ्य ( Fact ) — सामान्य तौर पर तथ्य का अर्थ वर्तमान वस्तु से है जिसका मनुष्य का बोध हो सकता है तथा इसमें वे वस्तुएँ सम्मिलित नहीं होती जो मनुष्य के मस्तिष्क से सम्बन्धित हैं परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई तथ्य की परिभाषा सिर्फ बोधगम्य या दृश्यमान (tangible) वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। उसमें कथन, भावनाएँ (emotions), विचार (thought) तथा मानसिक अवस्थाओं को भी भौतिक तथ्यों की भाँति तथ्य माना गया है।
साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार तथ्य शब्द के अर्थ के अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया गया है-
(1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो तथा
(2) कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो।
इस प्रकार इस धारा में दी गई तथ्य की परिभाषा में भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इस धारा में दी गई परिभाषा के अनुसार तथ्य में वस्तु की सभी अवस्थाएँ सम्मिलित हैं जो मनुष्य अपनी पाँचों इन्द्रियों द्वारा महसूस कर सकता है। यदि आलमारी में किताबें सजी हैं, यह एक तथ्य होगा क्योंकि उसे मनुष्य अपनी आँख द्वारा देख सकता है। इसी प्रकार यदि कोई शब्द मनुष्य सुन सकता है तो उस शब्द का होना एक तथ्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्पर्श इन्द्रिय द्वारा कुछ महसूस कर रहा है या घ्राण (सूँघकर) इन्द्रिय द्वारा किसी विशेष गंध को महसूस कर रहा है तो वह तथ्य है। उपरोक्त सभी उदाहरण भौतिक तथ्यों के हैं। परन्तु साक्ष्य अधिनियम में दी गई परिभाषाओं में मानसिक तथ्य भी सम्मिलित किया गया है अतः कोई व्यक्ति अमुक विचार रखता है यह एक तथ्य है। किसी व्यक्ति को कोई भावना है यह भी तथ्य है। जैसे—वैमनस्य, दुश्मनी, मुरे विचार, अच्छे विचार ये सभी तथ्य हैं।
इस प्रकार तथ्य दो प्रकार के होते हैं भौतिक तथा मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य का से है तथा सम्बन्ध जीवित या निर्जीव वस्तु से है तथा उसके अस्तित्व का बोध उसके गुणों से न होकर इससे होता है कि उसकी अन्य वस्तुओं से किस प्रकार सम्भाव्यता है। जैसे-घोड़ा, आदमी उन्हें बाह्य तथ्य (external facts) भी कहते हैं। कुछ सुनना, देखना, कुछ कहना ये सभी भौतिक तथ्य हैं। इसके विपरीत मानसिक तथ्यों का स्थान किसी जीवित वस्तु उसके गुण से है जिससे वह जीवित कहा जाता है। अतः इस प्रकार से तथ्य सिर्फ व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई अनुमति, याददाश्त, उसकी इच्छाएँ, उसका आशय सद्भाव, ज्ञान [उदाहरण (घ)]। या किसी व्यक्ति को कोई ख्याति है यह एक तथ्य है [उदाहरण (ङ)]। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं, यह एक तथ्य है।
(2) सुसंगत तथ्य (Relevant fact )- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब होगा जब वह एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हो या सम्बन्धित हो जैसा कि साक्ष्य अधिनियम के सुसंगतता के अध्याय में वर्णित है। दूसरे शब्दों में एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जायेगा जब वे आपस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक की धाराओं में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित हों। इस प्रकार सुसंगत शब्द के दो अर्थ हैं-
(1) सम्बन्धित होना या जुड़ा होना तथा (2) ग्राह्य होना।
सुसंगत तथ्य को समझाते हुए स्टीफेन महोदय कहते हैं कि यदि दो तथ्य आपस में कारण और प्रभाव के रूप में सम्बन्धित हैं तो वे सुसंगत होते हैं, परन्तु सुसंगत तथ्यों का वास्तविक अर्थ उस तथ्य से लिया जाना चाहिए जिसमें सम्भावना की शक्ति हो एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब होगा जब वे आपस में एक-दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित हों कि एक-दूसरे के अस्तित्व को या तो अत्यधिक सम्भव बनाते हैं या अत्यधिक असम्भव बनाते हैं। परन्तु साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत होने के लिए यह आवश्यक है कि वह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक में वर्णित तथ्यों से किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित हो या जुड़ा हो क्योंकि धारा 5 के अनुसार सिर्फ वही तथ्य सुसंगत होंगे जो इस अधिनियम के सुसंगतता के अध्याय में वर्णित विभिन्न प्रावधानों में से एक या अधिक से किसी न किसी प्रकार सम्बन्धित हैं क्योंकि किसी वाद या कार्यवाही में वही तथ्य न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जायेगा जो सुसंगतता के अध्याय में सुसंगत तथ्यों के रूप में वर्णित है अन्य नहीं। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम के अर्थों में सुसंगत तथा ग्राह्य तथ्य समानार्थी हैं। जो सुसंगत है वही ग्राह्य है वही सुसंगत है।
संक्षेप में एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब दो तथ्य आपस में किसी प्रकार से सम्पृक्त (जुड़े) हों। इस सामान्य घटनाक्रम के अनुसार यह तथ्य अकेले या दूसरे तथ्य के साथ मिलकर दूसरे तथ्य को (विवाद्यक तथ्य को) साबित करता हो या दूसरे तथ्यों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के अस्तित्व को अत्यधिक सम्भव या असम्भव बनाते हों। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब नहीं होगा जब इनमें सम्बन्ध दूरस्थ (Remote) हों या जब ऐसे तथ्य को विचार में लेने पर दूसरे तथ्य (विवाद्यक तथ्य) का साक्ष्यिक मूल्य कम हो जाता है।
उदाहरण के लिए धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति का तर्क है। यह तथ्य कि ‘अ’ घटनास्थल से बहुत दूर कलकत्ता में घटना के समय था तथा घटना वाराणसी में हुई, उस तथ्य को असम्भव बनाता है कि ‘अ’ ने वाराणसी में हत्या की थी। अतः यह एक सुसंगत तथ्य होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने हित के प्रतिकूल स्वतन्त्रतापूर्वक कोई कथन करता है तो इसकी सम्भावना अधिक है कि वह सत्य बोलता है अतः स्वीकृति तथा संस्वीकृति सूचक तथ्य ग्राह्य होते हैं।
क्या न्यायालय लोकनीति के आधार पर संसुगत तथ्यों की अवहेलना कर सकता है— एक कहावत है “Salus Poluli Est Supreme Lex”, जिसका अर्थ यह है कि लोकहित ही सर्वोपरि कानून है। दूसरे शब्दों में लोकनीति के आधार पर न्यायालय द्वारा सुसंगत तथ्यों को भी ग्राह्य करने से इन्कार किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान ऐसे उपलब्ध हैं जिनके अन्तर्गत पक्षकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे कुछ साक्ष्य प्रस्तुत न करने के विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। (धारा 122, 123, 126 ) । धारा 122 में वैध विवाद के दौरान पति-पत्नी के मध्य गुप्त संसूचनाओं के बारे में यह अधिकार प्राप्त है। धारा 123 में राज्य के कार्यों से सम्बन्धित उक्त दस्तावेज के बारे में तथा धारा 126 के अन्तर्गत एक अभियुक्त (मुवक्किल) को यह विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त धारा 167 में यह प्रावधान है कि किसी सुसंगत तथ्य का न्यायालय द्वारा ग्राह्य न किया जाना अपने आप में नवीन वाद का आधार नहीं होगा।
(3) साबित (Proved ) – एक तथ्य साबित किया हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालय या तो तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास कर ले या उस तथ्य का अस्तित्व न्यायालय इतना सम्भाव्य मान ले कि कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी उन्हीं परिस्थितियों में इस अनुमान पर पहुँचे कि उस तथ्य का अस्तित्व रहा होगा। [ धारा 3]
इस प्रकार साबित’ शब्द की परिभाषा में दो प्रकार की मनः स्थितियाँ दी गई हैं-
(1) वह जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य की यथार्थता पर पूर्ण विश्वास करता है;
(2) वह जब उसे ऐसा विश्वास तो नहीं होता किन्तु उस तथ्य के सत्य होने की सम्भावना की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति उसे तथ्य
मानकर उसके अनुकूल आचरण करने में संकोच नहीं करता।
उदाहरण के लिए कत्ल के मुकदमें में चार गवाह आँखों देखा साक्ष्य देते हुए अभियुक्त धारा 164, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपराध इकबाल करता है। उसके शरीर से खून से कपड़े मिलते हैं। सबूत पर विचार करते हुए यह विश्वास के योग्य है कि अभियुक्त ने ही कत्ल किया है।
‘सबूत (Proof)’ शब्द का तात्पर्य किसी ऐसी चीज से है जो किसी तथ्य या मान्यता की सत्यता या असत्यता के बारे में मस्तिष्क को समझा सके। सबूत साक्ष्य का परिणाम है। साक्ष्य साबूत का एक माध्यम है। इस प्रकार साक्ष्य यदि स्वीकार कर उस पर विश्वास कर लिया जाय तो उसका परिणाम सबूत होता है। परन्तु साक्ष्य अपने आप में सबूत नहीं है। इस प्रकार स्वाक्ष्य (Evidence) तथा सबूत (Proof) पर्यायवाची ( Synonym) या समानार्थी नहीं हैं। एक-दूसरे का प्रभाव या परिणाम हैं सबूत का तात्पर्य गणित जैसी कठोर साबित (Strict Proof) से नहीं है क्योंकि ऐसा कर पाना असम्भव होगा। सबूत के लिए इतना ही साक्ष्य पर्याप्त होगा जिससे एक युक्तियुक्त (Reasonable) बुद्धि के व्यक्ति के मस्तिष्क को किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस प्रकार साक्ष्य और सबूत एक नहीं है, एक माध्यम है तो दूसरा प्रभाव या परिणाम है।
आपराधिक तथा दीवानी कार्यवाहियों में सबूत के बारे में अन्तर- दीवानी तथा आपराधिक कार्यवाही सम्भवतः पक्षकारों के लिए समान है परन्तु सबूत को लेकर इन कार्यवाहियों में भिन्नता है। दीवानी या व्यावहारिक कार्यवाहियों में सबूत इस सीमा तक पर्याप्त है कि न्यायालय को किसी (विवाद्यक) तथ्य की सम्भाव्यता या असम्भाव्यता के बारे में विश्वास हो जाय। परन्तु आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त को अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में दीवानी मामलों में सबूत सम्भाव्यता के स्तर तक आवश्यक होता है जबकि आपराधिक कार्यवाहियों में कठोर सबूत का नियम लागू होता है अर्थात् आपराधिक कार्यवाहियों में जुर्म को सम्भावना निश्चितता की सीमा तक साबित की जानी चाहिए।
किसी तथ्य को साबित हुआ मानने के लिए साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषय भी सम्मिलित हैं जिन पर न्यायालय ध्यान देता है जो साक्ष्य की परिभाषा के अन्तर्गत तो सम्मिलित नहीं की गई है परन्तु ये किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में न्यायालय को विश्वास दिलाती हैं। जैसे- न्यायालय द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट, साक्षियों की तथा पक्षकारों को स्वीकृतियों, अभियुक्त का कथन, ये साबित हुआ कि परिभाषा में प्रयुक्त “न्यायालय के समक्ष अन्य विषयवस्तु” (other matter before Court) शब्दावली के अन्तर्गत सम्मिलित है।
( 4 ) नासाबित (Disproved ) — ना साबित शब्द पूर्व चर्चित ‘साबित’ शब्द का प्रतिरूप (विलोम) है। कोई तथ्य नासाबित तब कहा जाता है जब दोनों पक्षकार या एक पक्षकार किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देते हैं किन्तु न्यायालय का विचार है कि उन साक्ष्यों द्वारा विवादपूर्ण तथ्य के अस्तित्व का विश्वास नहीं हो पाया। कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय या तो-
(क) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन तथ्य का अस्तित्व नहीं है या
(ख) उसके अस्तित्व के न होने की इतनी अधिक सम्भावना है कि उन परिस्थितियों में किसी भी साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कथित तथ्य वर्तमान नहीं है। [ धारा 3]
जैसे ‘अ’ पर हत्या का आरोप है तथा ‘अ’ यह सिद्ध कर दे कि जिस तिथि को हत्या हुई थी वह उस तिथि को जेल में बन्द था। इस साक्ष्य से यह विश्वास करना सम्भव नहीं हो पायेगा कि ‘अ’ हत्या के समय हत्या के स्थान पर उपस्थित रहकर हत्या कर सकता है।
यहाँ पक्षकार ऐसा सकारात्मक सबूत पेश करता है जिससे विवाद्यक (मुख्य) तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता। इस प्रकार यदि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस निश्चय पर पहुँचे कि विवाधक तथ्य का अस्तित्व सम्भाव्य नहीं है तो यह कहा जाएगा कि तथ्य नासाबित हुआ।
यहाँ यह स्मरणीय है कि किसी तथ्य को नासाबित तब कहा जायेगा जब उसके अस्तित्व के बारे में सम्भाव्यता को नकारने वाले सकारात्मक साक्ष्य (तथ्य) प्रस्तुत कर दिये गये हैं। जैसे अन्यत्र उपस्थिति का तर्क, तथ्य को असम्भाव्य बनाने वाले तथ्य।
(5) साबित नहीं हुआ (Not Proved) – जब बाद या कार्यवाही के पक्षकार किसी विवादित तथ्य को न तो स्थापित कर पाते हैं या न ही नासाबित या असिद्ध ही कर पाते हैं तो यह कहा जाता है कि वह तथा साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ साबित तथा नासाबित के बीच की स्थिति है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय के समक्ष किसी मामले में किसी विवाधक तथ्य को साबित करने हेतु प्रस्तुत किये गये तथ्य उस तथ्य को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं होते तथा दूसरे पक्षकार द्वारा उस विवाद्यक तथ्य को नासाबित (असिद्ध) करने हेतु पेश किये गये तथ्य ( साक्ष्य) भी पर्याप्त नहीं होते तो यह कहा जायेगा कि वह तथ्य साबित नहीं हुआ (The fact is not proved) ।
इस प्रकार साबित नहीं हुआ (Not proved) एक संशय की स्थिति है जिसमें न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर न तो इस विश्वास पर पहुँचता है कि विवाद्यक तथ्य साबित हुआ तथा न ही इस विश्वास पर पहुँच पाता है कि तथ्य नासाबित है।
ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि तथ्य साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि तथ्य साबित नहीं हुआ। उदाहरण के रूप में ‘क’ पर ‘ख’ की हत्या का आरोप है। अभियोजक यदि साबित करने में सफल हो जाता है कि ‘क’ ने ‘ख’ की हत्या की तो यह कहा जायेगा कि तथ्य साबित हुआ। यदि ‘क’ यह साबित करने में सफल हो जाता है कि घटना के समय वह जेल में था तो यह कहा जायेगा कि तथ्य नासाबित हुआ। परन्तु यदि दोनों ओर का साक्ष्य, न्यायालय के अनुसार विश्वास योग्य नहीं है तो यह कहा जायेगा कि तथ्य साबित नहीं हुआ।
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ‘साबित नहीं हुआ’, साबित (Proved) और नासाबित (Disproved) के बीच की मानसिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में ठीक-ठीक कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि तथ्य साचित हुआ है या नासाबित।
प्रश्न 3. (i) उपधारणा से आपका क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है? What do you understand by Presumption? What are its kinds?
(ii) उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा तथा निश्चयात्मक सबूत पदावली का अर्थ स्पष्ट करें। Explain the meaning of the terms may presume, shall presume and conclusive proof.
उत्तर (i) – सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक तथ्य जिनके आधार पर पक्षकार न्यायालय का निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं साबित किए जाने चाहिए। परन्तु साक्ष्य विधि, न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में किन्हीं तथ्यों को साबित किये बिना ही विचारण में लेने की अनुमति देती है अर्थात् साक्ष्य विधि के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा किन्हीं तथ्यों की उपधारणा किये जाने का प्रावधान है। उपधारणा (Presumption) शब्द से तात्पर्य है किन्हीं तथ्यों का अनुमान कर लेना। किन्हीं ऐसे तथ्यों के आधार पर (जैसे न्यायिक सूचना, या स्वीकृत तथ्यों या किन्हीं तथ्यों को साबित कर दिये जाने पर) किसी अन्य तथ्य के अस्तित्व के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक अनुमान (Inference) ही उपधारणा है। उपधारणा का आधार मानवीय अनुभव तथा प्राकृतिक नियम होते हैं। उदाहरण के रूप में ‘अ’ की साइकिल खो गई है जो खोने के तत्काल पश्चात् ‘व’ के पास पाई गयी। यहाँ इस तथ्य से दो अनुमान निकलते हैं। प्रथम यह कि बने अ की साइकिल चुराई होगी और दूसरे यह कि उसने यह जानते हुए कि साइकिल चोरी की है, प्राप्त की होगी। एक पत्र उचित पता लिखकर डाक में डाला गया इससे यह अनुमान होता है कि वह पत्र जिसे प्रेषित किया गया है, प्राप्त हो गया होगा। प्रकृति के नियम के आधार पर यह उपधारणा होती है कि रात के पश्चात् दिन होता है। वर्षा ऋतु के पश्चात् शरद ऋतु आती है।
संक्षेप में कहें तो उपधारणा किसी अज्ञात तथ्य के बारे में कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर निकाला जाने वाला अनुमान है जिसका आधार मानवीय अनुभव तथा प्रकृति के नियम होते हैं। या दूसरे शब्दों में “यह एक अनुमान है जो विपरीत साक्ष्य न मिलने पर किया जाता है।”
उपधारणा दो प्रकार की होती है- (1) तथ्य की उपधारणा (Presumption of fact ) तथा (2) विधि की उपधारणा (Presumption of Law)।
(1) तथ्य की उपधारणा (Presumption of fact) – तथ्य की उपधारणा वह अनुमान है जो कि किसी अज्ञात तथ्य के बारे में ज्ञात तथ्यों के आधार पर मानवीय अनुभव तथा प्रकृति के नियम के आधार पर लगाया जाता है। तथ्य की उपधारणा का आधार मानवीय तर्क (Logic) होता है। मानवीय अनुभव के अनुसार एक तथ्य का अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को तार्किक रूप से सम्भव बनाता है।
मनुष्य की मानसिक स्थिति आशय, ज्ञान या सद्भाव को साबित करना कठिन है इसका अनुमान अभियुक्त के कार्य-कलापों के आधार पर किया जाता है। जैसे क पर यह आरोप है कि उसने ख को आशयपूर्ण ढंग से गोली मारकर हत्या की है। क का कहना है कि हत्या दुर्घटनावश हुई। यह तथ्य अज्ञात है कि क का ख की हत्या का आशय था या नहीं। यह तथ्य अज्ञात है कि क ने ख पर प्रश्नगत अवसर के अतिरिक्त कई अन्य अवसरों पर उसकी हत्या करने के लिए गोली चलाई थी परन्तु ख बच गया था। क के पूर्ववर्ती आचरण के आधार पर उसके ख को मारने के आशय के बारे में उपधारणा की जा सकती है। धारा 114 से जुड़े दृष्टान्त तथा धारा 86, 87, 88 तथा धारा 90 तथ्य की उपधारणा के उदाहरण हैं। तथ्य की उपधारणा सदैव खण्डनीय होती है।
(2) विधि की उपधारणा (Presumption of Law) – विधि की उपधारणा वे धारणायें हैं जो विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं। ये विधि को उपधारणाओं का उचित तर्क न होकर विधि के प्रावधान होते हैं। विधि की उपधारणाएँ खण्डनीय (Rebuttable) तथा अखण्डनीय (Imebutable) दोनों प्रकार की होती है।
खण्डनीय उपधारणाओं के उदाहरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 107, 108 तथा 112 में मिलते हैं। धारा 107 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को पिछले 30 सालों में देखा गया है या उसके बारे में सुना गया है तो उसके जीवित होने की उपधारणा की जायेगी तथा धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बारे में पिछले सात सालों में कुछ नहीं सुना गया है या उसे देखा नहीं गया है तो यह उपधारणा होगी कि वह मर गया है। धारा 107 में जीवित होने की उपधारणा तथा धारा 108 में मृत्यु की उपधारणा का खण्डन ठोस सबूत द्वारा किया जा सकता है। ऐसा करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा करना चाहता है। इसी प्रकार धारा 112 में वैध विवाह के दौरान उत्पन्न सन्तान की औरसता (Legitimacy) के बारे में उपधारणा किये जाने का प्रावधान है।
अखण्डनीय उपधारणाओं के उदाहरण धारा 115, 116 तथा 117 हैं। धारा 41 में न्यायिक निर्णय किसी व्यक्ति की विधिक स्थिति के बारे में अखण्डनीय उपधारणा किये जाने का प्रावधान है। अखण्डनीय उपधारणा, निश्चयात्मक सबूत होते हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार सात वर्ष के बालक के बारे में निश्चयात्मक उपधारणा है कि यह अपराध नहीं कर सकता।
सैय्यद अकबर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए० आई० आर० 1979 एस० सी० 1848 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि की उपधारणाओं के मामले में न्यायालय का विवेक नहीं होता है और न्यायालय तथ्य को साबित तौर पर उपधारित करने के लिए बाध्य है जब तक कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे नासाबित या खण्डन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाता है।
उत्तर (ii) उपधारित करेगा, उपधारित कर सकेगा तथा निश्चयात्मक सबूत (Shall Presume, May Presume and Conclusive Proof)— साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 उपधारित करेगा, उपधारित कर सकेगा तथा निश्चयात्मक सबूत शब्दावली की परिभाषा देती है। हराधन मेहता तथा अन्य बनाम दुखु मेहता, ए० आई० आर० 1993 इलाहाबाद 119 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारित कर सकेगा शब्दावली का प्रयोग कर न्यायालय को किसी तथ्य को उपधारित करने या न करने का विवेक दिया गया है जहाँ उपधारित करेगा, शब्दावली का प्रयोग किया गया है वहाँ कुछ तथ्य को उपधारित करने के लिए विधायी आदेश दिया गया है। यहाँ न्यायालय को विवेक (Discretion) प्राप्त नहीं है। कुछ तथ्य के सबूत के पश्चात् कुछ उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है।
उपधारित करेगा (Shall Presume ) — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 79, 80, 81, 83, 89, 104, 105, 107, 108, 112 तक की धाराओं में (Shall Presume) उपधारित करेगा’ शब्दावली का प्रयोग है। ये शब्द यह प्रदर्शित करते हैं कि यदि कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया है (जाता है) तो न्यायालय यह उपधारित करने के लिए बाध्य है कि जो तथ्य सम्बन्धित धारा में वर्णित हैं उनका अस्तित्व है। ये धाराएँ निदेशात्मक (Directive) हैं न कि अनुज्ञात्मक (Permissive)।
उपधारित कर सकेगा (May Presume ) — धारा 86 से 88 तथा धारा 90, 114, 118 में उपधारित कर सकेगा शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिसके अनुसार इन धाराओं में वर्णित मामलों में न्यायालय को यह विवेक दिया गया है कि यदि न्यायालय उचित समझे तो उपधारणा कर सकता है अथवा पक्षकारों को, दस्तावेज को साक्ष्य के माध्यम से साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है अर्थात् जिन धाराओं में (May Presume) “उपधारित कर सकेगा” शब्दावली का प्रयोग है, ये धाराएँ निदेशात्मक (Directive) न होकर अनुज्ञात्मक (Permissive) हैं।
सीताराम बनाम ननकू, 2 ए० एल० जे० 833 के मामले में कहा गया कि अदालत यह उपधारित कर सकती है कि जो व्यक्ति किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और वह स्वेच्छा से करता है।
निश्चयात्मक सबूत (Conclusive Proof) – सामान्य नियम के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में विचारित तथ्यों के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा सकारात्मक (Positive) सबूत देकर साबित करना पड़ता है या उस तथ्य को असिद्ध करने के लिए सकारात्मक सबूत देने होते हैं। कुछ मामलों में यदि कतिपय ज्ञात तथ्यों को साबित कर दिया जाय तो विधि न्यायालय को अधिकार देती है कि वह अज्ञात विवादित तथ्य के बारे में अनुमान लगाए या अनुमान (उपधारणा) लगा सके। परन्तु साक्ष्य अधिनियम में किन्हीं किन्हीं धाराओं में निश्चयात्मक सबूत का प्रयोग किया गया है। जैसे धारा 41 के अनुसार जहाँ सक्षम न्यायालय द्वारा वैवाहिक क्षेत्राधिकार में अन्तिम आदेश, निर्णय या आज्ञप्ति पारित की गई है तो यह निर्णय इत्यादि उस व्यक्ति के विधिक चरित्र के निश्चयात्मक सबूत हैं जिनके बारे में यह निर्णय, आजति या आदेश पारित किया गया है।
यहाँ इस धारा में निश्चयात्मक सबूत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। निश्चयात्मक सबूत का तात्पर्य यह है कि न्यायालय किसी ऐसे साक्ष्य को पेश किये जाने पर, जो किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है, किसी अन्य साक्ष्य की माँग नहीं करेंगी तथा उसे पेश किये गये साक्ष्य के प्रश्नगत तथ्य के सन्दर्भ में निश्चयात्मक मान लेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी विधिक निर्णय या आज्ञप्ति या आदेश में किसी व्यक्ति के विधिक चरित्र का निश्चयात्मक सबूत घोषित किया गया है तो उस निर्णय आदि को पेश किये जाने पर उस व्यक्ति के विधिक चरित्र के बारे में किया गया निर्णय स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्य विकल्प नहीं है। न्यायालय पक्षकारों से इस विधिक चरित्र को साबित करने हेतु अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने का आग्रह नहीं कर सकती है।
‘निश्चयात्मक सबूत’ का प्रयोग धारा 112 के अन्तर्गत भी किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता तथा किसी पुरुष के वैध विवाह के दौरान होता है। तो यह निश्चयात्मक सबूत होगा कि वह व्यक्ति उसी पुरुष की वैध सन्तान है। यदि कोई सन्तान विवाह विच्छेद के 280 दिन के अन्दर माता के अविवाहित रहने पर उत्पन्न होतो है तो यह भी सन्तान की औरसता का निश्चयात्मक सबूत होगा।
प्रश्न 4. निम्न में अन्तर स्पष्ट करें।
(i) तथ्य एवं साक्ष्य
(ii) तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणा
(iii) मेडिकल साक्ष्य और पारिस्थितिक साक्ष्य
Differentiate between the following.
(i) Fact and Evidence
(ii) Presumption of fact and Presumption of Law
(iii) Medical Evidence and Circumstantial Evidence
उत्तर (i) – तथ्य एवं साक्ष्य में अन्तर (Difference between Evidence & Fact)
साक्ष्य (Evidence)
(1) साक्ष्य वह साधन है ( गवाह तथा दस्तावेज) जिसके द्वारा सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है।
(2) साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी हो सकते हैं।
(3) साक्ष्य को अभिव्यक्त रूप में होना आवश्यक है। मानसिक तथ्य तभी साक्ष्य हो सकता है जब उन्हें अभिव्यक्त किया गया हो।
(4) सभी साक्ष्य किसी न किसी प्रकार के तथ्य अवश्य होते हैं ।
तथ्य ( Fact )
(1) तथ्य वह है जिसका कि अस्तित्व है या जिसका मनुष्य को ज्ञान है।
(2) तथ्य सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकते हैं।
(3) तथ्य भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं अर्थात् किसी व्यक्ति का विचार या आशय तथ्य हो सकते हैं।
(4) सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं होते जब तक उन्हें किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय अपने समक्ष पेश करने की अनुमति न प्रदान करता हो।
उत्तर (ii)- तथ्य की उपधारणा तथा विधि की उपधारणा में अंतर (Difference between Presumption of fact and Presumption of law)
तथ्य की उपधारणा (Presumption of fact )
(1) तथ्य की उपधारणा का आधार तर्क है ।
(2) तथ्य की उपधारणा की स्थिति अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होती है ।
(3) तथ्य की उपधारणा जूरी द्वारा की जाती है तथा सदैव खण्डनीय होती है ।
(4) तथ्य की उपधारणा चाहे जितनी भी सशक्त हो न्यायालय उनकी उपेक्षा कर सकता है।
(5) तथ्य की उपधारणा प्राकृतिक नियमों, मानवीय अनुभवों तथा प्रचलित प्रथाओं के आधार पर निकाली जाती है।
विधि की उपधारणा (Presumption of law)
(1) विधि की उपधारणा विधिक नियमों के आधार पर लगाई जाती है।
(2) विधि की उपधारणा की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है।
(3) विधि की उपधारणा न्यायालय द्वारा की जाती है तथा खण्डन के अभाव में निश्चयात्मक होती है।
(4) विधि की उपधारणाओं की उपेक्षा न्यायालय नहीं कर सकता।
(5) विधि की उपधारणा न्यायिक नियमों के स्तर पर प्रतिष्ठित है और विधि का भाग बन गई है।
उत्तर (iii) मेडिकल साक्ष्य और पारिस्थितिक साक्ष्य में अन्तर (Variance between Medical Evidence and Circumstantial Evidence) – स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एच० कोरोजीनायक (1995) कर्नाटक के बाद में जहाँ कि विष से मृत्यु के प्रश्न में मेडिकल साक्ष्य ने विष से मृत्यु नहीं साबित किया परन्तु अन्य परिस्थितियों में अभियुक्त के दोष का समर्थन किया। अभिनिर्धारित हुआ कि अभियुक्त को दोषसिद्ध किय जा सकता है यद्यपि मेडिकल साक्ष्य नकारात्मक था।
एक अन्य वाद स्टेट ऑफ केरल बनाम मनी, (1932) क्रि० लॉ० ज० 1682 (केरल) में जहाँ शव परीक्षा करने वाला डॉक्टर मृत्यु के कारण के बारे में निश्चित राय देने की स्थिति में नहीं था। अभिनिर्धारित हुआ कि न्यायालय अभियुक्त को पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध कर सकता है।
प्रश्न 5. (i) तथ्यों की सुसंगति से आप क्या समझते हैं? “सुसंगति” और “ब्राह्मता” में अन्तर कीजिए। What do you under stand by ‘Relevancy of Facts’? Bring out difference between “Relevancy” and “Admissibility”?
अथवा
जो सुसंगत है, वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होता, किन्तु जो ग्राह्म होता है, वह सुसंगत है। समझाइये। All admissible evidence are relevant but all relevant evidence are not necessarily admissible. Comment.
(ii) रेस गेस्टा या रेस जेस्टा पदावली से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित अपने उत्तर को समझाइए ।
अथवा
एक ही संव्यवहार के निर्माण करने वाले तथ्य किन परिस्थितियों में सुसंगत माने गये हैं। अपने उत्तर को उदाहरण सहित समझाइये।
Explain the term Res-Gestae with illustration.
Or
When and under what circumstances the facts forming part of same transaction are relevant? Explain your answer with example.
उत्तर (i)—सुसंगत तथ्य ( Relavant fact) – भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य की परिभाषा नहीं दी गयी है। धारा 3 में केवल यह कहा गया है कि-
“एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।”
जब दो तथ्य एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं तो उन्हें सुसंगत कहते हैं। उनमें इस प्रकार का सम्बन्ध होता है कि एक को जानने के लिए दूसरे तथ्य का जानना सहायक होता है।
“सुसंगत तथ्य वे तथ्य होते हैं जो किसी विवाद में विवाद्यक तो नहीं होते, परन्तु विवाद्यक तथ्य के अस्तित्व की सम्भावना को प्रभावित करते हैं और उनका प्रयोग विवाद्यक तथ्य के बारे में अनुमान के लिए किया जा सकता है।” किसी विवाद्यक तथ्य को साबित करने के लिए उससे सम्बन्धित कुछ अन्य तथ्यों का साबित किया जाना जरूरी हो सकता है क्योंकि वे विवाद्यक तथ्य से सम्बन्धित हो सकते हैं। परन्तु यह आवश्यक है कि सम्बन्ध धारा 6 से धारा 55 के अनुसार ही होना चाहिए। अन्यथा किसी तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सुसंगत नहीं माना जा सकता।
उदाहरण- यदि ‘अ’ पर आरोप है कि उसने ‘ब’ को लूटा, तो विवाद्यक तथ्य तो यह होगा कि क्या ‘अ’ ने ‘ब’ को लूटा पर उस मुकदमें में यह तथ्य कि ‘अ’ को लूटने के स्थान पर जाते हुए देखा गया। दूसरे दिन जब ‘अ’ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, ‘स’ के यह कहते ही कि रात में किसी ने ‘ब’ को लूटा था और पुलिस लुटेरे की खोज में इधर ही आ रही है, ‘अ’ आधी कप चाय छोड़कर चल दिया, सुसंगत तथ्य होगा, क्योंकि उसका सम्बन्ध विवाद्यक तथ्य से है और वह सम्बन्ध साक्ष्य अधिनियम के अनुसार है।
सुसंगति तथा ग्राह्यता में अन्तर
सुसंगति और ग्राहता में अन्तर होता है। कभी-कभी इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में लोग लेते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सुसंगति का अर्थ होता है एक तथ्य का दूसरे तथ्य के सम्बन्ध और ग्राह्यता का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। यह आवश्यक नहीं है कि सभी सुसंगत तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य हों और न तो यही आवश्यक है कि सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत हाँ। जैसे- यदि किसी पति ने अपराध करने के बाद अपनी पत्नी से अपराध करना स्वीकार किया है तो इससे अधिक सुसंगत तथ्य और क्या हो सकता है, पर इस तथ्य पर साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि धारा 122 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पति द्वारा पत्नी से किया गया कथन साक्ष्य में नहीं ग्रहण किया जा सकता। इसी प्रकार कुछ ऐसे तथ्य भी साक्ष्य में ग्रहण किये जा सकते हैं जो सुसंगत न हों। जैसे-यदि कोई साक्षी अपना कथन करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है तो उसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो अधिनियम के अनुसार सुसंगत न हों। यदि बाद रुपये के लेन-देन से सम्बन्ध रखता है और गवाह की विश्वनीयता पर आक्षेप करने के लिए उससे पूछा जाता है कि अब तक वह चोरी के मामले में कितनी बार जेल जा चुका है तो इस प्रश्न के उत्तर का कोई सम्बन्ध विवाद्यक तथ्य से न होते हुए भी साक्ष्य में ग्राह्य होगा।
दूसरा अन्तर जो किसी तथ्य के सुसंगत और ग्राह्य होने में है वह यह है कि किसी तथ्य की सुसंगति के लिए वह आवश्यक है कि वह धारा 6 से 55 तक जो नियम दिये गये हैं उस प्रकार से सम्बन्धित हो और तथ्य की ग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि जिस तथ्य पर जो साक्ष्य दिया जा रहा हो वह किसी नियम के अधीन अग्राह्य न घोषित किया गया हो।
सुसंगतता तथा ब्राह्मता न तो पर्यायवाची है और न ही एक-दूसरे में सम्मिलित हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया है और इसलिए धारा 136 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है।
‘सुसंगति’ का अर्थ सम्बन्ध से होता है और वह सम्बन्ध धारा 6 से धारा 55 के अनुसार ही होना चाहिए। यदि कोई तथ्य उनमें से किसी धारा के अनुसार सुसंगत नहीं है तो उस पर साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धारा 5 में यह स्पष्टतया कहा गया है कि साक्ष्य के ऐसे तथ्यों पर दिया जा सकता है, जो या तो विवाधक हों या सुसंगत हो और किसी पर नहीं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि विधायक या सुसंगत तथ्य पर जो साक्ष्य दिया जा रहा हो वह साक्ष्य में पाढ़ा हो जब भी किसी मामले में न्यायालय के सामने कोई तथ्य साक्ष्य के रूप में पेश किया जायेगा तो पहला प्रश्न यही होगा कि क्या यह तथ्य किसी प्रकार से सुसंगत है। इसका उत्तर धारा 6 से धारा 55 तक में मिलेगा। यदि प्रश्न का उत्तर हाँ में होता है तो न्यायालय यह देखेगा कि क्या यह पास है? यदि ग्राह्य है तो न्यायालय उसे साक्ष्य में ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं। जैसे-यदि ‘अ’ ने ‘च’ पर यह दावा किया कि उसने प्रोनोट लिखकर ‘अ’ से 500 रुपये ऋण लिया और दिया नहीं। ‘अ’ प्रोनोट न्यायालय में दाखिल करता है पर उस पर टिकट नहीं है। अब यहाँ जहाँ तक सुसंगति का प्रश्न है प्रोनोट सुसंगत होगा पर साक्ष्य में प्राह्म नहीं होगा, क्योंकि बिना टिकट लगा प्रोनोट साक्ष्य में अग्राह्य होता है।
अतः किसी तथ्य का सुसंगत होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि उस तथ्य पर दिया जाने वाला साक्ष्य ग्राहा भी हो और साथ ही यह भी सही है कि कुछ तथ्यों पर साक्ष्य ग्रहण किये जा सकते हैं, यद्यपि ये तथ्य धारा 6 से 55 के अनुसार सुसंगत नहीं होते। इसलिए यह कहा गया है कि सुसंगति और ग्राह्यता सहव्यापक शब्द नहीं हैं।
उत्तर (ii)—रेस गेस्टा (Res-Gestae) – इस पदावली का प्रयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं किया गया है। यह पदावली अंग्रेजी साक्ष्य अधिनियम में प्रयोग की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में यह कहा गया है कि वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार के अंग (भाग या आवली) का निर्माण करते हैं तथ्य सुसंगत हैं। चाहे ये तथ्य एक स्थान पर घटित हुए हो या भिन्न-भिन्न स्थानों पर या एक ही समय घटित हुए हों या भिन्न-भिन्न समय पर इस प्रकार रेस गेस्टा जो अंग्रेजी विधि में प्रयुक्त है तथा एक ही संव्यवहार के निर्माण करने वाले तथ्य जिनका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लेख है, समानार्थी हैं।
रेस गेस्टा या एक ही संव्यवहार’ की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई हैं। स्टीफेन महोदय के अनुसार, “एक संव्यवहार” तथ्यों का वह समूह है जो आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि उन्हें अपराध या संविदा या अपकृत्य जैसे एक विधिक नाम को संज्ञा दी जा सके या जो विवादग्रस्त जाँच की विषय हो। संव्यवहार की ठीक-ठीक परिभाषा देना कठिन है परन्तु कोई तथ्य संव्यवहार का अंग है या नहीं इसे निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वे तथ्य आपस में वर्तमान निरन्तर कार्यकलाप के अंग के रूप में जुड़े हों।
रेस गेस्टा का अर्थ है “एक संव्यवहार” किया गया कार्य या विषय वस्तु सामान्य रूप से किसी मामले में रेस गेस्टा सांसारिक कार्यों का वह अंग है जिससे बाद या कार्यवाही में आरोपित अधिकार या दायित्वों का आवश्यक रूप से निर्धारण होता है। रेस गेस्टा शब्द का प्रयोग दी अर्थों में किया गया है। अपने समुचित अर्थ में रेस गेस्टा का अर्थ है सांसारिक कार्य- कलाप जिससे मनुष्य के दायित्व या अधिकारों का विनिश्चय होता हो अपने विस्तृत अर्थों में इसमें वे सभी सम्भावित तथ्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष संव्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ न्यायालय को संव्यवहार या घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते। विस्तृत अर्थों में रेस गेस्टा उन सभी तथ्यों को सम्मिलित करता है जो आरोपित मुख्य कृत्य या कार्यों के प्रारम्भ होने से उसके समाप्त होन तक घटित होते हैं। कृत्य या अपराध के (निरन्तर जारी होने (चालू रहते) के समय घटना से सम्बन्धित जो कुछ भी व्यथित व्यक्ति द्वारा या आस-पास मौजूद व्यक्तियों द्वारा घटना की निरन्तरता के दौरान कहा गया हो। मुख्य अपराध के रेस गेस्टा के रूप में या उस संव्यवहार में भाग के रूप में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकेगा। दूसरी ओर जब अपराधी द्वारा किये गये सभी कार्य समाप्त हो जायें उसके पश्चात् कुछ समय बीत जाने के पश्चात् व्यक्ति द्वारा यदि कुछ कहा जाय या आस-पास में लोग कुछ बात करें, वह रेस गेस्टा या एक ही संव्यवहार के अंग के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
उदाहरण के रूप में ‘अ’ सड़क पर एक तेज रफ्तार से जाती हुई ट्रक से घायल हो जाता है। ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर भाग गया। उसके तत्काल पश्चात् कुछ लोग घायल व्यक्ति के पास पहुँचते हैं उस समय घायल व्यक्ति द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है या आस-पास के व्यक्तियों द्वारा घटना के सम्बन्ध जो कुछ कहा गया है यह एक ही संव्यवहार के अंग या रेस गेस्टा के रूप में, साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा क्योंकि यहाँ घटना अभी निरन्तर थी। परन्तु यही व्यक्ति घर जाकर यदि घटना का विवरण प्रस्तुत करे या घटना समाप्त होने के पश्चात् घटना स्थान पर खड़े व्यक्ति आपस में जो कुछ भी कहते हैं वह रेस गेस्टा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। [आर० बनाम फोस्टर, (1834)]
जैसे- एक व्यक्ति एक महिला का गला काटकर भाग गया। गला काटते समय महिला न तो चिल्लाई, न शोर मचायी। परन्तु उसके कुछ समय पश्चात् घायल महिला घर से बाहर निकल कर घटना के सम्बन्ध में जो कुछ बताती है वह रेस गेस्टा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आर० बनाम वेडिंग्फील्ड, (1879 14 COX CC)
रतन सिंह बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1997 एस० सी० 768 नामक बाद में अभियुक्त एकाएक कमरे में घुसा तथा उसने अपनी बन्दूक से कान्तादेवी को मारा। हमले में पूर्व मृतका ने जो कुछ भी कहा उसका रेस गेस्टा के रूप में ग्राह्य किया गया। उच्चतम न्यायालय ने धारा 6 के उदाहरण (क) का दृष्टान्त देते हुए मृतक के कथन को धारा 6 के अन्तर्गत ग्राह्य किया।
जहाँ एक संव्यवहार कई भौतिक तथ्यों द्वारा निर्मित हैं, वहाँ उन तथ्यों की श्रृंखला (Chain) एक ही संव्यवहार का निर्माण करे, इसके लिए आवश्यक है कि वे तथ्य आपस में एक-दूसरे से समय की समीपस्थता (Proximate) तथा कार्यों की निरन्तरता एवं उद्देश्य के समुदाय से जुड़े होने आवश्यक हैं।
समय की समीपता (Proximity of Time) – आवश्यक यह है कि संव्यवहार को निर्मित करने वाले तथ्यों के बीच की कड़ी या श्रृंखला (Chain) भंग नहीं होनी चाहिए। यदि घटना को निर्मित करने वाले तथ्यों की कड़ी या श्रृंखला में व्यतिक्रम है तो न्यूनतम समय ही पर्याप्त होगा। एक महिला की हत्या के लिए अभियोजन में महिला के हमलावर भाग गये उसके तुरन्त पश्चात् महिला ने अपनी घायलावस्था में टेलीफोन आपरेटर से पुलिस को फोन मिलाने को कहा, आपरेटर ने पुलिस को फोन मिलाया इतने में ही घायल महिला मर गयी तथा फोन कट गया। आपरेटर ने पुलिस को महिला का पता बताया। महिला द्वारा आपरेटर को घटना के सम्बन्ध में जो कुछ बताया गया था, घटना के तारतम्य में ही था। अतः एक ही संव्यवहार के अंग होने के कारण सुसंगत माना गया। रटन बनाम क्वीन, (1971)
इस प्रकार यहाँ यह आवश्यक है कि घटना के समाप्त होने के पश्चात् घटना के विवरण देने के समय में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए कि घायल व्यक्ति या सूचना देने वाले को कुछ सोचने का अवसर प्राप्त हो गया हो।
कृष्ण कुमार मलिक बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ए० आई० आर० (2011) एस सी० 2877 के बाद में बलात्कार से पीड़ित लड़की का यह आचरण अस्वभाविक था कि उसने अपने अपहरण के तथ्य को बहुत देर तक छुपा कर रखा, धारा में सुसंगत होने के लिए यह जरूरी है कि कथन घटना के साथ-साथ हुआ हो या उसके तुरन्त बाद।
संव्यवहार का अंग (भाग) निर्माण करने वाले तथ्य- यदि एक घटना हो रही है तो जो व्यक्ति घटना कर रहा है तथा जिसके प्रति घटना हो रही है या घटना स्थल पर खड़े व्यक्तियों द्वारा बोले गये शब्द एक ही संव्यवहार का अंग होने के कारण सुसंगत होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को चाकू मारा जा रहा है तो जो व्यक्ति चाकू मार रहा है उसके द्वारा बोले गये शब्द, जिसको चाकू मारा जा रहा है उसके द्वारा बोले गये शब्द या चाकू मारने की घटना के आस-पास मौजूद व्यक्तियों द्वारा बोले गये शब्द एक ही संव्यवहार का अंग होने के कारण सुसंगत होते हैं। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि इन कथनों को साथ-साथ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन कथनों के मध्य समय का अन्तराल इतना नहीं होना चाहिए कि कथनकर्ता को सोचने का अवसर मिल गया हो या कथन पिछली घटना की कहानी लगती हो। ये कथन तभी सुसंगत होंगे जब ये मुख्य कृत्य से प्रभावित लगते हों। जहाँ कही भी याददाश्त का प्रवेश होता जाता है। कथन सुसंगत नहीं होंगे।
एक कथन सिर्फ इसीलिए सुसंगत नहीं हो जायेगा कि वह घटना के समय बोला गया था, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह संव्यवहार का अंग हो। हादू बनाम राज्य, ए० ई० आर० 1957 उड़ीसा 53 के वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक ही संव्यवहार के आई० दृष्टान्त का हवाला दिया कि मान लो ‘अ’, ‘ब’ पर चाकू से हमला करता है जिसे देखकर ‘स’ चिल्लाता है-देखो वह चाकू से मार रहा है। यह एक ही संव्यवहार का अंग होने के कारण सुसंगत होगा। यह विस्मयकारक शब्द भी घाव से बहते रक्त की भाँति ही संव्यवहार का अंग होने के कारण सुसंगत होगा। यह विस्मयकारक शब्द भी घाव से बहते रक्त की भाँति ही संव्यवहार का अंग है। अन्तर सिर्फ यह है कि बहता रक्त कृत्य की भौतिक अभिव्यक्ति है तथा विस्मयकारक शब्द कृत्य की भावनात्मक या मानसिक अभिव्यक्ति है।
भौरव सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम० पी० ए० आई० आर० (2009) एस० सी० 2603 के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी कथन को किसी संव्यवहार का भाग माना जाय, इसके लिए यह जरूरी है कि बोले गये शब्द संव्यवहार के साथ-साथ हुए हों या पर्याप्त रूप से लगभग उसी समय हुए हों ताकि यह कहा जा सके कि ये संव्यवहार के दौरान या तुरन्त पहले या तुरन्त पश्चात् हुए हों। प्रस्तुत बाद में साक्षियों की गवाही जो मृतक स्त्री के बारे में थी जिससे उन्हें परिपीड़न एवं परेशानी का उन परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध ही नहीं था जिनके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी।
एक कथन को रेस गेस्टा के रूप में सुसंगत होने के लिए समवर्ती (Concurrent) होना चाहिए या इतने समय बाद कथन न किया गया हो जो कथन के पश्चात् घटना को कहानी बना देता हो। इस प्रकार घटना बीत जाने के पश्चात् प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया कथन रेस गेस्टा नहीं होगा। (प्रतापसिंह बनाम राज्य, 1971 क्रि० लॉ० ज० 172), जबकि एक हत्या के समय मारे जाने वाले व्यक्ति द्वारा बचाओं-बचाओं कहना तथा पास उपस्थित उसके बच्चों द्वारा चिल्लाना कि मेरी माँ को बचाओं, रेस गेस्टा के रूप में सुसंगत होगा- सावल दास बनाम बिहार, ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 778 धारा 6 से जुड़े दृष्टान्त विषय को और अधिक स्पष्ट करते हैं।
‘अ’ पर ‘ब’ को पीटकर मार डालने का आरोप है। पीटते के समय जो कुछ भी ‘अ’ द्वारा कहा या किया गया है तथा ‘ब’ द्वारा या आस-पास खड़े व्यक्तियों द्वारा घटना स्थल पर पीटते के समय या उसके कुछ समय पूर्व या पश्चात् कहा गया है। एक ही संव्यवहार का अंग होने के कारण सुसंगत होगा। दृष्टान्त (क)
सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध के लिए ‘अ’ पर आरोप है। इस युद्ध में सम्पत्ति नष्ट की जाती है, सेना पर हमला किया जाता है, जेल तोड़ी जाती हैं, ये सभी तथ्य एक ही संव्यवहार का निर्माण करने वाले तथ्य होने के कारण सुसंगत होंगे भले ही ‘अ’ उन सबमें उपस्थित न रहा हो। दृष्टान्त (ख)
‘अ’, ‘ब’ पर पत्र व्यवहार के अंग के रूप में एक पत्र द्वारा अपमानजनक कथन के लिए वाद लाता है। पक्षकारों के मध्य विषय से सम्बन्धित पत्र जिससे अपकथन (Libel) उत्पन्न हुआ है सुसंगत होंगे भले ही सभी पत्रों में अपकथन सन्निहित न हो। दृष्टान्त (ग)
जहाँ प्रश्न यह है कि कुछ सामान जिसमें सम्प्रदाय (Delivery) का आदेश ‘अ’ ने दिया था, ‘ब’ द्वारा ‘अ’ को प्रदान किया गया है या नहीं, यह तथ्य कि सामान कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया प्रत्येक सम्प्रदान (Delivery) सुसंगत होगा। दृष्टान्त (घ)
प्रश्न 6. (i) ऐसे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य के अवसर, कारण, प्रभाव, हेतु तैयारी या पक्षकारों के पूर्व एवं पश्चात्वर्ती आचरण हों कब तथा किस सीमा तक सुसंगत होते हैं?
When and upto what extent the Occasion, Cause, Effect, Motive, Preparation or Previous and Subsequent Conduct of parties are relevant?
(ii) विवाद्यक या किसी सुसंगत तथ्य की पृष्ठभूमि का निर्माण कराने वाले, स्पष्टीकरणात्मक, सम्पोषणात्मक, खण्डनात्मक तथा किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु की पहचान कराने वाले तथ्य की सुसंगतता का संक्षेप में विवेचन कीजिए।
Explain in short the relevancy of those facts which are necessary to introduce, explain, corroborate or rebutt the fact in issue or relevant fact and the fact which establish the identity of place, person or things.
(iii) षड्यन्त्र से आप क्या समझते हैं? षड़यन्त्र के मामलों में साक्ष्यों की ग्राह्यता सम्बन्धी नियमों का उल्लेख करें।
उत्तर (i)— प्रकृति का यह नियम तथा मानव अनुभव यह दर्शाते हैं कि समान घटनाएँ अपने कारणों तथा अवसरों एवं प्रभावों को एक समान प्रदर्शित करती हैं। एक हत्या वैमनस्य या दुश्मनी या रंजिश के कारण होती है तथा हत्या सुनसान स्थान आदि का अवसर तलाश कर की जाती है। सामान्यतया विभिन्न हत्याओं की घटनाओं के प्रभाव एक समान होते हैं। जैसे हत्या के स्थान पर अधिक मात्रा में मानवरक्त पाया जाना, हत्या के स्थान पर अस्तव्यस्त पदचिह्नों का मिलना तथा कभी-कभी खाली कारतूस का मिलना। यदि एक स्थान पर किसी मनुष्य या जानवर के या किसी वाहन के पहियों के चिह्न पाये जाते हैं तो सामान्य अनुभव से इसे किसी के गुजरने के प्रमाण (Proof) के रूप में लिया जाता है। चूँकि घटना के कारण, अवसर तथा प्रभाव उस घटना के घटित होने के तथ्य का अत्यधिक सम्भाव्यता प्रदान करते हैं अतः कारण, अवसर तथा प्रभाव को धारा 7 के अन्तर्गत माना गया है।
कारण (Cause) — प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मुकदमेबाजी या अन्य कारण से वैमनस्य, पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से प्रेम प्रसंग, कर्जदार से छुटकारा पाना, बलात्कार के मामले में बलात्कारी द्वारा बलात्कार की शिकार महिला की हत्या के पीछे साक्ष्य को नष्ट करना, कारण के रूप में सुसंगत होता है। किसी रेल दुर्घटना या विमान दुर्घटना के कारण की जाँच कारण के महत्व की ओर इशारा करती है।
‘अ’ तथा ‘ब’ दो मित्र थे, दोनों जुआ खेलते थे। इस प्रक्रिया में ‘अ’, ‘ब’ का काफी कर्जदार हो गया। ये दोनों मित्र साथ-साथ रहते थे। एक दिन ‘ब’ की लाश कमरे में मिली. तथा ‘अ’ फरार पाया गया। यहाँ यह सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है कि (यदि यह विवाद हो कि क्या ‘ब’ की हत्या ‘अ’ द्वारा की गई) ‘अ’ कर्ज से छुटकारा पाने के कारण ‘व’ की हत्या कर सकता है।
अवसर (Occassion) – सामान्यतः अपराधी अपराध करने के लिए सुअवसर या अनुकूल परिस्थितियों की तलाश करता है तथा अपराध अनुकूल परिस्थितियों में किये जाते हैं जिसमें अपराध के छुपाये जाने की अधिक से अधिक सम्भावना हो। इसे प्रसंग भी कहते हैं।
एक हत्या के विचारण में यह साक्ष्य दिया गया है कि जब मौसम बदली (Cloud) तथा तूफान का हुआ, बिजली गुल हो गई तथा चारों ओर अंधेरा हो गया तभी अवसर तलाशकर हत्या की गई यहाँ हत्या विवाद्यक तथा मुख्य तथ्य है तथा जिन परिस्थितियों में हत्या की गई यह अवसर या अनुकूल परिस्थितियों के होने के कारण सुसंगत होती है। इसी प्रकार डकैती तथा लूट भी सुनसान होने पर मध्यरात्रि के समय ही सामान्यतया होती हैं।
प्रश्न यह है कि क्या ‘अ’ ने ‘ब’ को लूटा? यह तथ्य कि लूट के कुछ समय पूर्व ‘ब’ रुपयों के साथ मेले में गया। ‘ब’ ने रुपया दिखाया तथा एक व्यक्ति से बताया कि वह रुपयों के साथ मेले में जा रहा है, अवसर के रूप में सुसंगत होगा। दृष्टांत (क)
आर० बनाम रिचर्डसन के वाद में यह तथ्य कि लड़की उस वक्त घर में अकेली थी, जिस समय उसकी हत्या की गई थी, सुसंगत था क्योंकि इससे हत्यारे को अवसर मिला था।
प्रभाव (Effect)—प्रत्येक घटनाएँ अपना प्रभाव अपने पीछे अवश्य छोड़ जाती हैं तथा अपने घटित होने की निशानी के रूप में सुसंगत होती हैं। इस विषय में स्पेन्सर कूपर का विचारण (Spencer Cooper’s Trial) महत्वपूर्ण है। इस बाद में प्रश्न था कि मृतक ने नदी में कूदकर आत्महत्या की या हत्या करके उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि मृतक के पेट में पानी नहीं था। अभियोजन पक्ष ने विशेषज्ञ की यह राय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी चाही कि यदि कोई व्यक्ति डूबने के कारण मरता है तो उसके पेट में पानी होना आवश्यक है। बचाव पक्ष इसके विरुद्ध तर्क देता है कि डूबकर मरने वाले व्यक्ति के पेट में पानी पाया जाना आवश्यक नहीं है। यहाँ यह सामान्य अनुभव है कि वाले व्यक्ति के पेट में पानी होता है अतः डूबकर मरने में प्रभाव के रूप में पेट में पानी पाया जाना धारा 7 के अन्तर्गत सुसंगत होगा।
इसी प्रकार विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों को भी प्रभाव के रूप में सुसंगत माना जाता है। प्रश्न यह है कि ‘अ’ ने ‘ब’ को विष देकर हत्या की। विष का प्रभाव जो मृतक के शरीर पर पाया गया सुसंगत होगा।
इस प्रकार विवाद्यक तथ्यों के कारण प्रभाव या उसे घटित होने में सुअवसर साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत, सुसंगत है।
प्रश्न यह है कि ‘अ’ ने ‘ब’ की हत्या की। हत्या के स्थान पर संघर्ष के निशान प्रभाव के रूप में सुसंगत होंगे। दृष्टांत (ख) धारा 7
टेप द्वारा अभिलिखित वार्तालाप इस धारा के अनुसार ग्राह्य है किन्तु यह सुनिश्चित होना
आवश्यक है कि-
(1) क्या यह वार्तालाप सुसंगत है;
(2) क्या आवाज की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है;
(3) क्या टेप वार्तालाप में गड़बड़ी होने वाली त्रुटियों को ध्यान में रखा गया है।
आर० एम० मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 157.
सुअवसर (Opportunity) — जो परिस्थितियाँ मुख्य तथ्यों को घटित होने का सुअवसर प्रदान करती हैं, उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करना चाहता है जो उसके सामान्य जीवन के अनुक्रम का भाग नहीं है उसे ऐसे कार्य के लिए सुअवसर बनाना पड़ेगा। आर० बनाम डोनेलन के बाद में मृतक को कब्ज की शिकायत रहती थी और इसलिए वह कभी-कभी शाम के समय जुलाब की एक खुराक लेता था। प्रायः उसकी माँ उसको यह खुराक देती थी। अभियुक्त को यह सब मालूम था। उसने खामोशी से जुलाब की शीशी के स्थान पर विष की शीशी रख दी। माँ ने न जानते हुए अपने ही हाथों से अपने ही लड़के को यह जहर पिला दिया जिससे वह मर गया। यह तथ्य कि अभियुक्त मृतक की आदतों से परिचित था, सुसंगत माना गया, क्योंकि इसी से उसे जहर इतनी आसानी से पिला देने का सुअवसर मिला था।
हेतुक, तैयारी तथा पक्षकारों के पूर्व तथा पश्चात्वर्ती आचरणों की सुसंगतता- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 विवाद्यक तथ्य के हेतुक, तैयारी तथा पक्षकारों के पूर्व तथा पश्चात्वर्ती आचरणों की सुसंगतता पर प्रकाश डालती है।
प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई प्रेरणा या हेतुक होता है। हेतुक के अभाव में कोई कार्य सम्पादित नहीं होता है क्योंकि हेतुक ही वह प्रेरणा या बल है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। इस प्रकार यह विनिश्चित करने हेतु कि क्या किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा नहीं प्रथमतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस कार्य को करने में उस व्यक्ति को क्या रुचि (Interest) या हेतु रहा होगा। जब यह साबित हो जाय कि उस कार्य को करने में उसका कोई हेतु था तब दूसरा प्रश्न यह है कि उस हेतु को कार्यान्वित करने हेतु उस व्यक्ति ने क्या तैयारी या योजना बनाई और इसी सन्दर्भ में उस व्यक्ति का पूर्व आचरण सुसंगत हो जाता है। कार्य सम्पादित करने के पश्चात् उस कार्य को छिपाने हेतु या उसके परिणामों से बचने हेतु वह व्यक्ति कोई कार्य करता है उस कार्य पश्चात् के रूप में (सुसंगत) महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
हेतुक का अर्थ (Meaning of Motive)- हेतुक या प्रेरणा वह बल है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य करने हेतु चलायमान या गतिशील करती है। हेतुक या प्रेरणा का स्थान व्यक्ति का मस्तिष्क होता है और यही हेतुक (Motive) या प्रेरणा व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश या प्रेरित करती है किसी कार्य की प्रेरणा या हेतुक को उत्पन्न करने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाना, बदला लेने की भावना, किसी से अवैध या दूषित सम्बन्ध या किसी के प्रति कर्ज या अन्य दायित्वों से छुटकारा प्राप्त करने का दबाव या किसी बुरी (दूषित) मनोदशा को पूर्ण करना आदि महत्वपूर्ण होते हैं।
हेतुक का सबूत — निःसन्देह हेतुक किसी वाद में महत्वपूर्ण अवश्य है परन्तु उसे साबित करना उतना ही कठिन है। इसीलिए यद्यपि हेतुक महत्वपूर्ण अवश्य है परन्तु कोई कार्य किया गया है अथवा नहीं उसे साबित करने के लिए हेतुक या प्रेरणा का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। जार्ज तथा अन्य बनाम केरल राज्य, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 1251 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक बार यदि अभियुक्त की अपराध में भागीदारी प्रत्यक्ष गवाह द्वारा सिद्ध हो जाय तो हेतुक का अभाव इसे दोषमुक्त नहीं कर सकता। नारायण बनाम महाराष्ट्र, ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1956. परन्तु यदि यह आरोप लगाया गया है कि कोई कार्य किसी विशिष्ट हेतुक या प्रेरणा के अन्तर्गत किया गया है तब हेतुक या प्रेरणा का सबूत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ भी जहाँ मामले का (कृत्य का) कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होता वहाँ भी हेतुक का सबूत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ अभियोजन किसी कार्य को करने में अभियुक्त का हेतुक साबित करने में असफल रहता है। और अभियुक्त द्वारा उस कार्य का किया जाना सन्देहपूर्ण है, वहाँ अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार यदि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि अभियुक्त ने एक विशिष्ट कार्य किया है, वहाँ हेतुक के सबूत का अभाव अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में अड़चन उत्पन्न नहीं कर सकता -राजेन्द्र कुमार बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1322.
हेतुक की पर्याप्तता – हेतुक या प्रेरणा की पर्याप्तता के बारे में सभी मामलों के लिए समान नियम लागू नहीं किया जा सकता है। यह अभियुक्त के चरित्र पर निर्भर करेगा क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति को अपराध करने के लिए कोई हेतुक प्रेरित नहीं कर सकता। परन्तु एक भ्रष्ट या अनैतिक व्यक्ति, तनिक या अल्प हेतुक के अन्तर्गत भी हत्या कर सकता है। परन्तु हेतुक या प्रेरणा किसी कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कार्य करने के पूर्व हेतुक या प्रेरणा उत्पन्न होने के कारणों के बावजूद व्यक्ति के पास पश्चाताप करने के अवसर होते हैं।
तैयारी का अर्थ (Meaning of Preparation) – साधारणत: हेतुक या प्रेरणा के जन्म लेने के पश्चात् व्यक्ति उसको मूर्त रूप देने के लिए साधन जुटाने की योजना बनाता है। इस प्रकार की तैयारी किसी अपराध या कार्य को करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की योजना है। हेतुक की भाँति तैयारी भी अपराध या कृत्य हो जाने के पश्चात् ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि तैयारी करने के पश्चात् भी व्यक्ति पश्चाताप के बाद अपना इरादा बदल लेता है। अपराध को करने तथा अपराध को छुपाने हेतु या अपराध से बचने हेतु किया गया कार्य भी तैयारी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, एक वाद में प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत दस्तावेज की वसीयत है या नहीं। यह तथ्य कि वसीयत के कुछ ही समय पूर्व ‘अ’ ने अपनी सम्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी उसने वसीयत करने हेतु वकील से सम्पर्क किया तथा वकील से कुछ वसीयतों में प्ररूप बनवाये थे जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था ये सभी तथ्य तैयारी के रूप में सुसंगत होंगे। दृष्टांत (घ) धारा 8
‘अ’ पर ‘ब’ की हत्या जहर देकर करने का आरोप है। यह तथ्य कि ‘व’ की मृत्यु के पूर्व ‘अ’ ने उसी प्रकार का विष प्राप्त किया था जो ‘व’ को मारने हेतु प्रयोग किया गया था तैयारी के रूप में सुसंगत होगा।
पक्षकारों के आचरण (Conduct of Parties) — किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद या कार्यवाही के हितबद्ध व्यक्तियों के आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का पैरा दो पक्षकारों के विवाद्यक तथ्य से सम्बन्धित आचरण को सुसंगत घोषित करता है। यहाँ पक्षकारों का अर्थ दीवानी कार्यवाही में वादी तथा प्रतिवादी एवं आपराधिक कार्यवाही में अभियोजन तथा अभियुक्त से है। आचरण एक व्यक्ति के गुणों को ऐसी बाह्य अभिव्यक्ति है जो कुछ न कुछ प्रभाव उत्पन्न करती है ये प्रभाव एक प्रकार के चिह्न होते हैं। जिनसे हम गतिमान होने के कारण अनुमान लगा सकते हैं। एक व्यक्ति के आचरण में वह सब सम्मिलित है जो वह करता है या करने में चूक करता है। जैसेकि धारा 8 के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि आचरण कुछ परिस्थितियों में कथन को भी सम्मिलित करता है ।
यह स्मरणीय है कि किसी वाद या कार्यवाही के पक्षकार के आचरण को सुसंगत होने के लिए यह आवश्यक है कि आचरण विवादित तथ्य या वाद या कार्यवाही के सन्दर्भ में हो। एक डकैती के वाद में अभियुक्त के संकेत पर कुछ धन पुलिस ने बरामद किया था। यह धन उसके विरुद्ध अभियोजन से सम्बन्धित नहीं था अतः यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं हुआ।
किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के सन्दर्भ में उस व्यक्ति द्वारा किया गया आचरण उसके विरुद्ध सुसंगत होने के कारण ग्राह्य होगा। जैसे ‘क’ पर जहर देकर हत्या करने। का आरोप है। ‘क’ द्वारा मृतक के शरीर की चिकित्सीय परीक्षा को टालने का प्रयत्न करने वाला आचरण सुसंगत होगा। उसी प्रकार ‘अ’, ‘ब’ के घर से गायब हुआ जब वह ‘ब’ के घर रहता था। ‘अ’ पर हत्या का आरोप है। इसके घर की फर्श खोदने का प्रयास करने पर उसके द्वारा आपत्ति की जाती है। इसके बावजूद फर्श खोदने का प्रयास होता है। ‘ब’ द्वारा फर्श खोदने