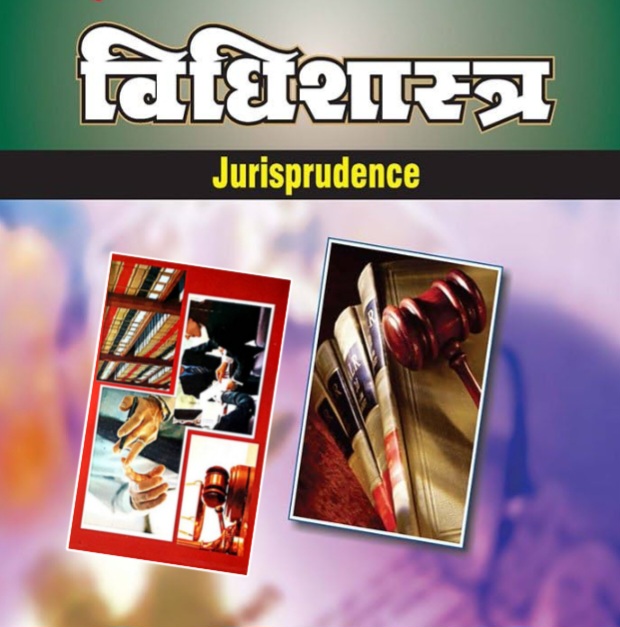-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-
प्रश्न 1. विधिशास्त्र के अर्थ तथा विस्तार को परिभाषित कीजिए। इसकी प्रकृति एवं उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। Define the meaning and scope of Jurisprudence. Assess its importance and nature.
अथवा (OR)
‘विधिशास्त्र’ को परिभाषित करें। इसकी प्रकृति तथा इसके क्षेत्र (विस्तार scope) को निर्धारित करें। Define ‘Jurisprudence’. Determine its nature and scope.
अथवा (OR)
डॉo हालैण्ड विधिशास्त्र को “सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान’ कहते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? Dr. Holland defines “Jurisprudence as a formal Science of Positive Law.” Do you agree with this view?
अथवा (OR)
विधिशास्त्र की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र के निर्धारण के बारे में किन्हीं दो विधिशास्त्रियों के विचारों की विवेचना कीजिए। इस सन्दर्भ में विशिष्ट विधिशास्त्र की अवधारणा के सम्बन्ध में ऑस्टिन एवं हालैण्ड के मतों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। Discuss the views of any two jurists about the definition of Jurisprudence and its scope of study. In this context make a comparative analysis of the view of Austine and Holland about the concept of particular Jurisprudence.
अथवा (OR)
“विधिशास्त्र का क्षेत्र निर्धारित तथा पुनः निर्धारित किया जाता रहा है क्योंकि इसके विषय-वस्तु की प्रकृति ही ऐसी रही है कि इसके क्षेत्र का कोई निर्धारण अन्तिम नहीं हो सकता है।”-डायस के इस कथन की समीक्षा करते हुए विधिशास्त्र का क्षेत्र निर्धारित कीजिए। “Province of Jurisprudence has been determined and redetermined and this is because of the nature of subject is such that no determination on its scope can be regarded as final.”-Dias. Discuss the statement and determine the scope of Jurisprudence.
अथवा (OR)
विधिशास्त्र के अर्थ तथा विस्तार को परिभाषित कीजिए। क्या आप जुलियस स्टोन के इस विचार से सहमत है कि विधिशास्त्र विधिवेत्ता का बहिर्गमन (Extra version) है। Define the meaning and scope of Jurisprudence. Do you agree with the view of Jullius Stone that Jurisprudence is the lawyers Extra-version.
अथवा (OR)
विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा दी गयी परिभाषाओं के आलोक में विधिशास्त्र की विवेचना कीजिए। सामण्ड के अनुसार “विधिशास्त्र ऐसा विषय है जिसे लागू नहीं किया जा सकता।” तब फिर हम क्यों इसका अध्ययन करते हैं? Discuss Jurisprudence in the light of definitions given by various jurists. According to Salmond “Jurisprudence is a subject without applicability.” Why should we study it then?
उत्तर – विधिशास्त्र की प्रकृति एवं विस्तार (Scope) — विधिशास्त्र की प्रकृति एवं विषय- -वस्तु कानून के अन्य विषयों से भिन्न होती है जिस प्रकार अन्य विधियों से सम्बन्धित कानून को पुस्तकों में एकरूपता होती है। लेखकों के विचार कुछ भी क्यों न हो किन्तु अधिनियमित कानून की विषय-वस्तु एक समान ही होगी। परन्तु विधिशास्त्र अधिनियमित विधि न होने के कारण उसकी विषय-वस्तु को अपने वैयक्तिक विचारों के अनुसार प्रस्तुत करने को स्वतन्त्रता विधिवेत्ताओं की होती है। विधिशास्त्र के अन्तर्गत विभिन्न कानूनों सम्बन्धी अवधारणाओं की विवेचना की जाती है जिनमें अधिकार, दायित्व, स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य, वैधानिक व्यक्तित्व, आशय, उपेक्षा (negligence) आदि के सामान्य एवं व्यापक स्वरूप का निरूपण किया जाता है।
विधिशास्त्र के क्षेत्र विस्तार के विषय में विधिवेत्ताओं ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। विधिशास्त्र द्वारा विधिशास्त्र के विस्तार का विनिर्धारण समय-समय पर उनके समक्ष विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार किया गया है। विधिशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे किसी निश्चित परिसीमा या विस्तार क्षेत्र में नहीं सीमित किया जा सकता। केल्सन ने विधिशास्त्र को नीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र से अलग रखा है। पाउण्ड (pound) के अनुसार विधिशास्त्र का क्षेत्र निर्णयों के सन्दर्भ में विधि का अध्ययन करना है। ऑस्टिन के विचार से विधिशास्त्र का क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। निश्चयात्मक विधि से उनका अभिप्राय उस विधि से है जो राज्य के सम्प्रभुताधारी शासक द्वारा नागरिकों के प्रति लागू की जाती है अर्थात् राज्य द्वारा प्रवर्तित विधि के अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिये। जबकि सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र का क्षेत्र नागरिक विधि के अध्ययन तक सीमित है। नागरिक विधि से उनका आशय विभिन्न देशों की नागरिक विधि के मूलभूत सिद्धान्तों से है इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने इस शास्त्र के प्रति अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं।
देखा जाय तो सामाजिक विकास तथा परिवर्तनों के साथ-साथ विधि सम्बन्धी धारणाएँ बदलती रहती हैं, परिणामतः विधि का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। अतः विधिशास्त्र के अन्तर्गत ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, दार्शनिक, चिकित्सकीय आदि ऐसे समस्त शास्त्रों का समावेश है जिनका उद्देश्य विधि सम्बन्धी धारणाओं तथा सिद्धान्तों का क्रियात्मक अध्ययन करना है। यही कारण है कि विधिशास्त्र का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा व्यापक है।
विधिशास्त्र की परिभाषा (Definition of Jurisprudence) — विधिशास्त्र विधि का दर्शन है (Jurisprudence is the Phylosophy of Law) यही इसकी प्रकृति की परिवर्तनशीलता का रहस्य है। चूँकि विभिन्न कालखण्डों में एक समरूप दर्शन की विचारधारा की कल्पना असम्भव है। अतः विधिशास्त्र का विभिन्न कालखण्ड में समरूप अर्थ, प्रकृति तथा सीमा हो। यह न तो उपक्रम है न ही विभिन्न कालखण्ड में विधिशास्त्र के एक रूप (uniform) अर्थ, प्रकृति, विस्तार या परिसीमा की कल्पना करना उचित ही है। यही कारण है कि यह प्रश्न उचित नहीं है कि विभिन्न कालखण्ड में विधिशास्त्र क्या है परन्तु प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक परिवेश तथा कालखण्ड में किन-किन वस्तुओं को विधिशास्त्र की संज्ञा दी जाती है।
विधिशास्त्र, ज्यूरिसप्रुडेन्स शब्द का पर्यायवाची है। Jurisprudence” (ज्यूरिसप्रुडेन्स) या विधि का ज्ञान या विधि का विज्ञान कौशल, लैटिन शब्द Juris तथा Prudentia के समतुल्य है। (Juris) का अर्थ है विधि (Law) तथा Prudentia (प्रुडेन्सिया) का अर्थ है ज्ञान (अरिस) (Knowledge)। रोमन लोगों के समय में ज्यूरिस प्रुडेन्सिया या विधिशास्त्र की परिकल्पना का उदय नहीं हुआ था प्राचीन विधिशास्त्री अल्पीयन (Ulpian) ने अपनी (डाइजेस्ट) पुस्तक में कहा है कि विधिशास्त्र देवी तथा माननीय वस्तुओं की परिकल्पना तथा उचित – अनुचित का ज्ञान है (Jurisprudence is the concept of things and human. the science of just and unjust), किसी समय विधिशास्त्र शब्द का प्रयोग विधि की किसी विशिष्ट शाखा की परिकल्पना के वर्णन के प्रयोजन से किया जाता था जैसे-साम्या विधिशास्त्र का प्रयोग विधि की साम्या (Equity) शाखा के वर्णन के लिए किया जाता था। कभी-कभी किसी विशिष्ट विषय के ज्ञान के सन्दर्भ में भी विधिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे चिकित्सा विज्ञान की शाखा को अभिव्यक्त करने के लिए चिकित्सीय विधिशास्त्र (Medical Jurisprudence) शब्द का प्रयोग किया जाता था। फ्रांस में किसी विशिष्ट न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्मित विधि के संग्रह के लिए भी विधिशास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्राथमिक काल में बेन्थम तथा उसके शिष्य ऑस्टिन के समय में विधिशास्त्र शब्द को ब्रिटिश विधिवेत्ताओं के मध्य तकनीकी अर्थ प्राप्त हुआ। ऑस्टिन लन्दन विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर (आचार्य) था ऑस्टिन को अंग्रेजी विधिशास्त्र का जनक (पिता) कहा जाता है। सन् 1945 में ऑस्टिन की अप्रकाशित पुस्तक “विधिशास्त्र की सीमाओं का परिनिर्धारण” (The Limits of Jurisprudence Defined) का प्रकाशन हुआ। ऑस्टिन द्वारा अभिव्यक्त विधिशास्त्र की परिकल्पनाएँ आज भी ब्रिटेन में अंग्रेजों के मध्य मान्यता तथा स्वीकृति प्राप्त है। इसीलिए आज भी इंग्लैण्ड में विधिशास्त्र के अर्थ तथा परिसीमा में आत्यन्तिक रूप में विधि तथा इसकी परिकल्पनाओं के औपचारिक विश्लेषण को ही किया गया है।
विधिशास्त्र सकारात्मक विधि का वैज्ञानिक विश्लेषण है (Jurisprudence w the scientific analysis of positive law)-
ऑस्टिन की परिभाषा – ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र सकारात्मक (Positive) या अधिरचित (Enacted) विधि का विश्लेषण (analysis) है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि विधिशास्त्र अधिति विधि (ऐसी विधि जो संसद या विधायिका द्वारा पारित विधि है) का विश्लेषण है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को सकारात्मक (अधिरचित: Enacted) या Positive (पोजिटिव) विधि के दर्शन (Phylosophy) के रूप में परिभाषित किया ऑस्टिन के अनुसार विधि का अध्ययन या विधि का विश्लेषण विधि के उद्देश्यों या विधि पारित करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए (What law ought be) परन्तु विधि का अध्ययन अधिनियम के अन्तर्गत निहित विधि ही है। विधि जैसी है (Law as it is) ही, विधि के अध्ययन या विश्लेषण या निर्वाचन (Interpretation) की विषय-वस्तु है। ऑस्टिन के अनुसार अधिरंचित विधि (Positive Law) वह विधि है जिन्हें राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ (Political Superior) व्यक्ति द्वारा राजनैतिक रूप से अवर (Political inferior) व्यक्ति के लिए निरूपित किया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्रियों को विधि का अध्ययन करते समय विधि कैसी होनी चाहिए इससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए बल्कि विधि का अध्ययन विधि निरूपित है वैसी ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पोस्टल अधिनियम में डाक कर्मियों की उपेक्षा के लिए निर्धारित प्रतिकर 500/- है तो न्यायाधीश अधिकतम 500/- रुपया प्रतिकर ही दिला सकता है। उसे यह अधिकार नहीं है कि यह इस मामले में यह देखे कि डाक कर्मियों की उपेक्षा से कथित पक्षकार को कितनी क्षति हुई है। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र, विधि का नैतिक दर्शन (Moral phylosophy) नहीं है परन्तु विधिशास्त्र विद्यमान, वास्तविक तथा अधिरचित (सकारात्मक: Positive) विधि का वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध (सुव्यवस्थित) अध्ययन (विश्लेषण) है। ऑस्टिन विज्ञान का विद्यार्थी था अतः ऑस्टिन ने विधि के विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical study) पर अधिक बल दिया। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्रियों को विधि का उसी प्रकार विश्लेषण करना चाहिए जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी रासायनिक पदार्थ का विश्लेषण करता है। उसे रासायनिक पदार्थ के बाह्य परिवेश से कोई प्रयोजन नहीं है।
ऑस्टिन का विशिष्ट एवं सामान्य विधिशास्त्र
ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को दो भागों में बाँटा है। एक विशिष्ट विधिशास्त्र (Particular Jurisprudence) तथा दूसरा सामान्य विधिशास्त्र (General jurisprudence)। सामान्य विधिशास्त्र से ऑस्टिन का तात्पर्य उन सिद्धान्तों, धारणाओं तथा परिकल्पनाओं की व्याख्याओं से है जो सभी विधि व्यवस्थाओं (Legal System) में समान रूप से पाये जाते हैं। इस प्रकार की विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वे विधि व्यवस्थाएँ आती हैं जो व्यापक (Universal) तथा परिपक्व (Mature) है।
विशिष्ट विधिशास्त्र (Particular Jurisprudence) से ऑस्टिन का तात्पर्य ऐसे विधिशास्त्र से है जिसके अन्तर्गत किसी विशिष्ट स्थान या समाज का कालखण्ड की विधि व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऐसी विधि-व्यवस्था किसी विशिष्ट समाज-राष्ट्र या कालखण्ड तक सीमित है। जैसे भारतीय विधि-व्यवस्था या अफ्रीका के किसी विशिष्ट समुदाय की विधि-व्यवस्था या किसी समय खण्ड में विद्यमान विधि व्यवस्था।
हालैण्ड की विधिशास्त्र की परिभाषा (Holland’s Definition of Jurisprudence)
थामस अस्काइन हालैण्ड (Thomas Erskine Holland) एक ब्रिटिश विधिशास्त्री था। धामस हालैण्ड ने ऑस्टिन की विधिशास्त्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाया। हालैण्ड ऑस्टिन के इस दृष्टिकोण से सहमत था कि विधिशास्त्र, विधि का वैज्ञानिक विश्लेषण (Scientific analysis) है। हालैण्ड ने विधिशास्त्र की छः शब्दों की परिभाषा “विधिशास्त्र अधिरचित (सकारात्मक) विधि का औपचारिक विज्ञान” (The formal science of positive law) दी। हालैण्ड स्वीकार करते हैं कि विधिशास्त्र अधिरचित (सकारात्मक: Positive) विधि का विज्ञान है परन्तु हालैण्ड के अनुसार यह औपचारिक विज्ञान (Formal Science) का विज्ञान है।
हालैण्ड के अनुसार, “विधिशास्त्र उन मानवीय सम्बन्धों का औपचारिक विज्ञान है जिनके लिए यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि उनके विधिक प्रभाव होते । हैं-अधिरचित विधि का औपचारिक विज्ञान”।
“The formal science of those relations of mankind which are generally recognised as having legal consequence-The Formal Science of Positive Law”,’
ऑस्टिन की भाँति अधिरचित विधि से हालैण्ड का तात्पर्य वास्तविक तथा वर्तमान विधि से है न कि काल्पनिक आदर्श (Hypothetical Morals) या अमूर्त विधि (Conceptual law) से।
हालैण्ड ने औपचारिक विज्ञान (Formal Science) को स्पष्ट करते हुए कहा कि औपचारिक विज्ञान वह है जिससे विधि में अन्तर्निहित मूलभूत सिद्धान्तों की विवेचना होती है। औपचारिक विज्ञान भौतिक (Physical) या पार्थिव विज्ञान नहीं है जिसमें ठोस विवरणों की विवेचना रहती है। हालैण्ड के अनुसार विधिशास्त्र का सम्बन्ध किसी विधिक सिद्धान्त के सामान्य भाग से होना चाहिए। विधिशास्त्र मानवीय सम्बन्धों (Human relations) की विवेचना करता है न कि भौतिक नियमों की या गुरुत्वाकर्षण या रासायनिक परिवर्तन से सम्बन्धित नियमों की।
हालैण्ड ने ऑस्टिन के विधिशास्त्र के विशिष्ट तथा सामान्य वर्गों के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए कहा कि विधिशास्त्र को विज्ञान कहना ठीक है परन्तु इसे विशिष्ट विज्ञान कहना गलत है। हालैण्ड के अनुसार विधिशास्त्र सदैव सामान्य (General) होता है। हालैण्ड के अनुसार यदि विधिशास्त्र स्थानीय (Local) है तो इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। हालैण्ड के अनुसार विशिष्ट लोगों की विधि का अध्ययन सिर्फ आंकड़ों का संग्रह (Collection of datas) है। यह एक व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है परन्तु यह विधिशास्त्र की विषय-वस्तु नहीं हो सकती।
सामण्ड ने ऑस्टिन तथा हालैण्ड के विधिशास्त्र के वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया है।
विधिशास्त्र नागरिक (सिविल) विधि के प्रथम (प्राथमिक) सिद्धान्तों का विज्ञान है-
सामण्ड की परिभाषा (Salmond’s Definition)- सामण्ड ऑस्टिन तथा हालैण्ड के इस विचार को मान्यता देते हैं कि विधिशास्त्र एक विज्ञान है। परन्तु सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र सामान्य न होकर विशिष्ट (Particular) है। विधिशास्त्र एक विशिष्ट विधि व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों का अध्ययन है। सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र विधि की एक विशिष्ट शाखा का अध्ययन है जिसे सिविल या नागरिक विधि कहते हैं। सामण्ड विधिशास्त्र को एक विशिष्ट अधिरचित (सकारात्मक) विधि पद्धति के सन्दर्भ में परिभाषित करते हैं। सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र नागरिक विधि या दीवानी विधि (Civil Law) के प्रथम सिद्धान्तों का विज्ञान (Science of first principle of civil law) है। “प्रथम सिद्धान्त” शब्द से सामण्ड का तात्पर्य किसी विशिष्ट विधि के मौलिक सिद्धान्तों (Fundamental Principles) से है। किसी विधि पद्धति के मौलिक सिद्धान्त उस विधि पद्धति के गौण विधिक नियम (Subsidiary legal rules) या सिद्धान्तों से भिन्न है। सामण्ड यह स्वीकार करते हैं कि किसी विधि पद्धति के प्राथमिक सिद्धान्त तथा उस विधि के गौण नियम के मध्य विभाजन रेखा खींचना कठिन कार्य है। प्रथम सिद्धान्त तथा अवशिष्ट विधि में अन्तर स्तर (degree) का है न कि प्रकार (Kinds) का मौलिक सिद्धान्तों को परिभाषित करते हुए सामण्ड कहते हैं कि मौलिक सिद्धान्त वे मौलिक परकिल्पनाएँ तथा सिद्धान्त हैं जो किसी विधि के ठोस विवरण का आधार होती हैं। विधिशास्त्री को विधिशास्त्र में किसी नागरिक विधि के मौलिक सिद्धान्तों के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। विधिशास्त्र में किसी विधिक पद्धति के अवशिष्ट विधि के सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं होना चाहिए। (विधि व्यवस्था के अन्तर्गत जो अन्य नियम या सिद्धान्त हैं) नागरिक विधि या दीवानी विधि (Civil Law) से सामण्ड का तात्पर्य विधिशास्त्रियों की विधि (The law of jurist) से है न कि नैतिक विधि या धार्मिक (Religious) विधि से सामण्ड ने नागरिक विधि (Civil law) शब्द का प्रयोग इस बात पर बल देने के लिए किया है कि विधिशास्त्र का विज्ञान सामान्य न होकर सिर्फ विशिष्ट (Particular) होता है। नागरिक विधि से उनका तात्पर्य किसी देश या राष्ट्र की विधि से है। नागरिक विधि से यहाँ तात्पर्य किसी विशिष्ट देश या राष्ट्र के न्यायालयों द्वारा प्रशासित होने वाली विधि से है जिसमें उस देश की सांविधिक विधि (Statute Law) प्रथाएँ तथा न्यायिक विधायन सम्मिलित हैं।
सामण्ड ने विधिशास्त्र का वर्गीकरण दो दृष्टिकोणों से किया है। सामान्य अर्थों में विधिशास्त्र तीन प्रकार का है-
(1) विधिक
(2) विधिक इतिहास, तथा
(3) विधायन का विज्ञान।
विशिष्ट अर्थों में विधिशास्त्र तीन प्रकार का है-
(1) विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र,
(2) ऐतिहासिक विधिशास्त्र तथा
(3) नैतिक विधिशास्त्र ।
सामण्ड की आलोचना यह कहकर की जाती है कि उन्होंने विधिशास्त्र के विस्तार को विशिष्ट विधिशास्त्र तक सीमित कर दिया है।
सामण्ड को पुस्तक विधिशास्त्र (Jurisprudence) के 12 वें संस्करण (1966) में विधिशास्त्र को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है-
“विधिशास्त्र, विधि (law) के एक निश्चित प्रकार के अन्वेषण को दिया गया नाम है. यह अन्वेषण विधि के अमूर्त, सामान्य तथा सैद्धान्तिक स्वभाव के बारे में जिसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि विधि एवं व्यवस्था (Law and Legal System) आवश्यक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया जाय।” “Jurisprudence is the name given to a certain type of investigation into law, an investigation of an abstract, general and theoretical nature which seeks to lay.”
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विधिशास्त्र की एक सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना सम्भव नहीं है। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपने समय के समाज तथा कालखण्ड के सन्दर्भ में विधिशास्त्र को परिभाषित किया है। विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा दी गयी विधिशास्त्र की परिभाषा उनके कालखण्ड के लिए उपयुक्त (Suitable) थी परन्तु आज के सन्दर्भ में उनकी परिभाषा अनुपयुक्त ही नहीं निरर्थक भी है। इसीलिए बकलैण्ड (Buckland) ऑस्टिन के बारे में कहते हैं-
“मेरे युवा काल में ऑस्टिन की विधिशास्त्र की परिभाषा उस समय के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त थी। ऑस्टिन उस समय धर्म थे परन्तु आज वे रोग (बीमारी) हैं।” “The analysis of legal concept is what jurisprudence means for the student in days of youth. Infact it meant Austin. He was a religion today he seems to be regarded rather as religion.”
प्रोफेसर सी० के० एलन ने सामण्ड तथा हॉलैण्ड दोनों विधिशास्त्रियों की परिभाषाओं को अस्वीकार करते हुए कहा कि दोनों महान विधिशास्त्रियों ने विधि के अध्ययन के संश्लेषणात्मक (Synthetic) दृष्टिकोण की अनदेखी की है। सामण्ड विधिशास्त्र को एक विशिष्ट विधि तक सीमित करके अति संकुचित हो गये जबकि हॉलैण्ड ने एक विशिष्ट विधिक प्रणाली के अध्ययन को अधिक अनिश्चित बना दिया है। एलेन के अनुसार किसी विधिक प्रणाली या विधि को प्रभावित करने वाली सामाजिक आवश्यकताओं, हितों तथा बलों को पृथक रखकर विधि की परिकल्पनाओं के निचोड़ या सारांश के रूप में विधि का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः सामाजिक आवश्यकताएँ तथा सामाजिक हित विधिशास्त्र की विषय-वस्तु के रूप में सम्मिलित हैं। सी० के० एलन के अनुसार, विधिशास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण है (Jurisprudence is the scientific analysis of essential principles of law) वैज्ञानिक विश्लेषण से एलन का तात्पर्य | मौलिक विधिक सिद्धान्तों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन (Orderly and Systemactic study) से है विधिशास्त्र में गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक विज्ञान के सिद्धान्त का अध्ययन नहीं किया जाता।
पैटन के अनुसार, विधिशास्त्र विधि से सम्बन्धित एक अध्ययन है (Jurisprudence is the study relating to law), पैटन के अनुसार विधिशास्त्र अध्ययन का एक विशिष्ट तरीका है, किसी देश की विशेष विधि का नहीं अपितु विधि को सामान्य धारणा का।
विधिशास्त्र की आधुनिक परिकल्पना – विधिशास्त्र विधिवेत्ता का अतिरिक्त कथन है (Jurisprudence is lawyer’s Extra-version) – उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व विधिशास्त्र का सम्बन्ध दर्शन (Phylosophy), धर्म (Religion), नीतिशास्त्र (Morals) तथा राजनीति से रहा हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ऑस्टिन ने विधिशास्त्र में वैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति का समावेश किया तथा विद्यमान या वर्तमान विधि तक ही विधिक अध्ययन को सीमित रखने की संस्तुति की। ऑस्टिन के अनुसार, विधिशास्त्र का विषय विधि जैसी है (as it is) या सकारात्मक विधि से सरोकार नहीं होना चाहिए। विधिशास्त्र का सम्बन्ध विधि कैसी होनी चाहिए (Law ought to be) इस पर विचार नहीं होना चाहिए। बीसवीं शताब्दी के पदार्पण ने विधिशास्त्र की परिकल्पना में मौलिक परिवर्तन किया। विधिशास्त्र दार्शनिक धर्म गुरुओं तथा राजनीतिज्ञों की पकड़ से मुक्त हुआ तथा अब विधिशास्त्र विधिवेत्ताओं के अध्ययन का विषय बना। जूलियस स्टोन इस नवीन आधुनिक युग की विचारधारा के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरे। जूलियस स्टोन (Julius Stone) के अनुसार, विधिशास्त्र वकीलों (विधिवेत्ता) का अतिरिक्त कथन (Extra-version) है। अतिरिक्त कथन से तात्पर्य विधिवेत्ता द्वारा इतर विधाओं द्वारा (be Extra-Technic) निकले आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तकनीक, उसके आदशों एवं नियमों के परीक्षण से है। Lawyers extra-version is the lawyers examination of the precepts and technique of law in the light derived from present knowledge in discipline other than law)
स्टोन के अनुसार, विधिशास्त्र के अन्तर्गत विधि का अध्ययन विधिक परिकल्पनाओं के अतिरिक्त अन्य विधाओं (other descipline) के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। एक वकील या विधिवेत्ता विधि के अध्ययन में अन्य विधाओं (other descipline) का भी ध्यान रखता है। जैसे सामाजिक परिवेश, विधि के अन्तर्गत प्राप्त किया जाने वाला प्रयोजन तथा विधि की कठोर व्याख्या द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव आदि के सन्दर्भ में विधि का अध्ययन विधिशास्त्र की विषय-वस्तु है। विधि के प्रावधानों की व्याख्या करते समय एक विधिवेत्ता जिन अतिरिक्त परिकल्पनाओं को ध्यान में लेता है, वह अतिरिक्त कथन (Extra Version) भी विधिशास्त्र की विषय-वस्तु है। जैसे जमानत (Bail) के मामले में जमानत के सांविधिक आधारों (Statutory basis) के अतिरिक्त वकील को न्यायालय के समक्ष उन दुष्प्रभावों को भी रखना चाहिए जो अभियुक्त को जमानत न देने के कारण उसके परिवार पर पड़ता है। यही विधिवेत्ता का अतिरिक्त कथन है। स्टोन के अनुसार विधिशास्त्र की विषय-वस्तु विधिवेत्ता का अतिरिक्त कथन है।
जूलियस स्टोन की भाँति होम्स, पोलक, ब्रेण्डिस, कारडोजो, फ्रैंक तथा विनोग्रेडोफ जैसे आधुनिक विधिशास्त्रियों ने भी विधि को सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित किया। इनके अनुसार यदि विधिवेत्ता सामाजिक पृष्ठभूमि, नैतिक सन्दर्भ तथा राजनीतिक औचित्य के अभाव में विधि का अध्ययन करता है तो वह ऐसा अपनी जोखिम पर करता है क्योंकि किसी गम्भीर उपयोगी तथा वास्तविक विधिक कार्य के लिए समाज के विभिन्न पहलुओं तथा समाज की अन्य विधाओं का अध्ययन अपरिहार्य है। न्यायमूर्ति ब्रैण्डिस ने ठीक ही कहा है कि ऐसा वकील जिसने अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अत्यधिक सम्भव है वह विरोधी हो जाय। अतः एक वकील के लिए सामाजिक विधाओं (Social discipline) का अध्ययन अपरिहार्य है।
भारत में बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद करीम छागला, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर, न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपने निर्णयों में विधि की व्याख्या विधिवेत्ता के अतिरिक्त कथन की भावना के अनुरूप की है। इन न्यायमूर्ति ने विधि को सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय का साधन बनाया।
जिस प्रकार चिकित्सा मरीज के शारीरिक परीक्षण या उसके पूर्व पृष्ठभूमि तथा चिकित्सीय परीक्षण के परिणामों के अभाव में सफल नहीं होती इसी प्रकार विधि भी सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक विधाओं के अध्ययन के अभाव में प्रभावी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में विधिशास्त्र के अध्ययन को अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक सिद्धान्त जैसे सामाजिक विज्ञान से पृथक नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर तथा अमेरिकन विधिवेत्ता न्यायमूर्ति ओलिवर विल्डेल होम्स ने सामाजिक परिवेश वाले प्रगतिशील विधिशास्त्र पर बल दिया है।
विधिशास्त्र – भारतीय पहलू (Jurisprudence-An Indian Aspect)
(1) प्राचीन झुकाव (Ancient Trend)- भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व हमारे देश में विधिक पद्धति प्रथाओं में अन्तर्निहित नियमों के अनुरूप थी।
ये प्रथाएँ धर्म ग्रन्थों में प्रतिपादित नियमों से आधार तथा वैधता पाती थीं। राजा ही विधि के शासन का स्रोत था। राजा ही प्रजापालक तथा प्रजा का संरक्षक था। राजा ही कार्यपालिका का प्रमुख था। राजा धर्म के नियमों के अनुरूप शासन करता था। राजा ऑस्टिन का सम्प्रभु नहीं था, परन्तु अपने को धर्मानुसार प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इस प्रकार विधिक प्रणाली धर्म को ही सम्प्रभु मानकर संचालित की जाती थी। कोई भी शासक धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था।
(2) भारत में ब्रिटिश शासन तथा विधिशास्त्र (British Rule in India and Jurisprudence)- ब्रिटिशों ने अपनी विधिक पद्धति, अपनी भाषा तथा राजनैतिक पद्धति को मनमाने ढंग से भारत में लागू किया। ब्रिटिश शासकों ने भारत की तत्कालीन विधिक पद्धति तथा प्रधागत विधि तथा सांविधिक संस्थाओं का उपहास उड़ाया। अंग्रेजों के अनुसार तत्कालीन देशी विधि तथा विधिक पद्धति असभ्य, जंगली तथा क्रूरतापूर्ण थी जिसका संशोधन तथा पुनर्स्थापन समय की आवश्कयता थी। अंग्रेज शासकों ने ऑस्टिन के विधिशास्त्र के अनुरूप भारतीय विधिक पद्धति का परिमार्जन किया। अधिनायक वाद, पुलिस राज्य, लोक विरुद्ध तथा विदेशी विधि तथा न्यायिक पद्धति सभी का एक साथ प्रयोग भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपने दैवपिता ऑस्टिन के विधि की अधिरचित विधि (Positive Law) या सकारात्मक विधिशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार, अपनी विधिक पद्धति, विधि न्यायिक पद्धति तथा भाषा को भारत के लोगों पर लागू किया। इस प्रकार सन् 1947 पूर्व भारत में विधिवेत्ता, न्यायाधीश तथा विधि अध्यापकों ने समाज तथा विधि के अध्ययन (विधिशास्त्र) की पद्धति के रूप में ऑस्टिन के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व विधि निर्माण में भारतीय लोगों का योगदान नहीं था। तत्कालीन विधि आयोगों का गठन अंग्रेज सदस्यों से होता था। साम्या, न्याय तथा सद्भाव भारत में ब्रिटिश विधि तथा ब्रिटिश विधिक पद्धति को लागू करने का माध्यम तथा साधन बना। साम्या, न्याय तथा सद्भाव (Equity, Justice and Good Conscience) की आड़ में ब्रिटिश विधि भारत में प्रवेश कर गयी।
भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात् स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय जैसी परिकल्पनाएँ भारतीय विधिक पद्धति का आधार बने। अब भारतीय विधायिकाएँ (संसद तथा विधान सभाएँ) ऐसी विधियों को दण्डित करने की ओर अग्रसर हुई जिनका एक मात्र उद्देश्य हरिजन-गिरी जन का कल्याण था। भूमि सुधार अधिनियमों, राजा-रजवाड़ों की समाप्ति से संबंधित विधि तथा संविधान के कुछ प्रावधान समानता तथा कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रयोजन संजोये थे। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने संकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के बारे में यह निर्णय देकर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत (लोक कल्याण के लिए) संसद को संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार था। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के अनुरूप कार्य किया, जिसके अन्तर्गत विधि का अध्ययन समाज के हितों तथा आर्थिक हितों की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता। सन् 1978 के आपात काल के पश्चात् कालखण्ड में उच्चतम न्यायालय ने नया विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। बन्धुआ मजदूर वाद एवं फुटपाथ तथा झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों के हित से संबंधित वाद में उच्चतम न्यायालय ने समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के अनुरूप कमजोर वर्गों के पक्ष में लीक से हंकटर निर्णय दिया तथा एक नवीन विधिशास्त्र का सूत्रपात किया लोकहित के बाद की परिकल्पना ने भी यह प्रदर्शित किया कि उच्चतम न्यायालय उन लोगों के हितों के प्रति चितित है जिनके पास अपने हितों तथा अपने कष्टों को न्यायपालिका के समक्ष लाने के लिए आर्थिक स्रोत का अभाव था। पुलिस अत्याचार तक अपनी निर्धनता के कारण लम्बी अवधि तक जेलों में बंद व्यक्तियों को भी उच्चतम न्यायालय ने ऑस्टिन के अधिरचित विधि के विधिशास्त्र की अनदेखी कर नवीन विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उपचार प्रदान किया। आज भारत में समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के अन्तर्गत विधि का अध्ययन, न्याय पद्धति का संचालन तथा विधि निर्माण का कल्याणकारी वातावरण बना है।
विधिशास्त्र का उपयोग – विधिशास्त्र के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं-
(1) यह हमें विधि की प्रकृति का बोध कराता है। यह विधि के वास्तविक नियमों के अध्ययन और उनके आधारभूत सिद्धान्तों का अन्वेषण करने में सहायता करता है।
(2) यह विधि का वैज्ञानिक विकास करने में सहायक होता है।
(3) यह मस्तिष्क की आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करता है और विधिक अभिव्यक्तियों और शब्दावलियों का उचित बोध कराता है।
(4) विधिशास्त्र पर शोधों का समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही वे भी उनके आदर्शों से प्रभावित हो सकते हैं।
(5) विधिशास्त्र विधिक संकल्पनाओं (Concepts) को तर्कयुक्त बनाने (rationalise) वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में हमें समर्थ बनाता है।
(6) विधिशास्त्र का शिक्षात्मक (Educational) मूल्य भी है। विधिक संकल्पनाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण विधिज्ञों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता है और उनकी तर्क तकनीक को प्रखर बनाता है। यह उनकी वैयक्तिकता (individuality) और औपचारिकतावाद (Formalism) को दूर करने में सहायक होता है और उन्हें सामाजिक यथार्थों और विधि के कृत्यात्मक (Functional) पहलू पर केन्द्रित करने को प्रशिक्षित (Trained) करता है।
(7) विधिशास्त्र किसी निर्दिष्ट समाज में विधि के बुनियादी विचारों और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है।
प्रश्न 2. विधिशास्त्र की कौन-कौन सी प्रमुख शाखाएँ हैं? इनकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
What are the various schools of Jurisprudence? Give a brief characteristics of these schools.
उत्तर-विधिशास्त्र की प्रमुख शाखाएँ- विभिन्न कालों और देशों में विधिशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विधि के अध्ययन का प्रयत्न किया है। उन्होंने विधि की परिभाषा दी है, इसके स्रोतों और प्रकृति को निश्चित किया है और इसके प्रयोजन (purpose) और लक्ष्यों (aims) का विवेचन किया है। विधि के बारे में इस व्यवस्थित चिन्तन को ‘विधि- सिद्धान्त’ (legal theory) या ‘विधि-दर्शन’ (legal philosophy) कहा गया है। स्पष्टता और उनके दृष्टिकोणों को समझने में सुविधा के लिये ये विधिशास्त्री विधि के सम्बन्ध में अपने विचार के आधार पर, विभिन्न विचारधाराओं (schools) में विभाजित किये गये- ‘विधशास्त्र’ शब्द को इसके ‘विशिष्ट’ अर्थ में लेते हुए, उसने इस विषय का तीन शाखाओं में विभाजन किया है, अर्थात् ‘विश्लेषणात्मक’ (analytical), ‘ऐतिहासिक’ (historical) और ‘नीतिशास्त्र’ (ethical)। यह विभाजन ऊपर दिये गये विभाजन के अनुरूप हैं।
(1) व्याख्यात्मक या प्रणाली-बद्ध (Expository or systematic)- जो ऐसी किसी वास्तविक विधि की प्रणाली (legal system) के तत्वों (contents) का विवेचन करता है, जो कि किसी समय मौजूद हो, चाहे भूतकाल में या वर्तमान में।
(2) विधिक इतिहास (Legal history) – जो किसी विधि-प्रणाली के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया (process) का विवेचन करता है।
(3) विधान विज्ञान (Science of legislation)- इसका प्रयोजन ऐसी विधि बनाना है जैसी कि यह होनी चाहिए। यह विधि-प्रणाली के आदर्श भविष्य और उन प्रयोजनों का जिनके लिये इसका अस्तित्व होता है, वर्णन करता है।
सामण्ड ने इन तीन शाखाओं के क्षेत्र का भी वर्णन किया है। अपनी स्वयं की पुस्तक के बारे में वह कहता है कि “प्राथमिक रूप से और आवश्यक रूप से यह विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र पर एक पुस्तक है।” इस सम्बन्ध में यह उस विधि-दर्शन (legal philosophy) के जो कि यूरोपीय महाद्वीप में विद्यमान है और जो एक बड़ी सीमा तक अपने क्षेत्र और पद्धति में मुख्य रूप से नीतिशास्त्रीय है, मुकाबले में आंग्ल-विधि-दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति का अनुसरण करने का प्रयत्न करती है। वह आगे कहता है कि मैंने अपने अध्ययन में से ऐतिहासिक और नीतिशास्त्रीय पहलू को पूरी तरह बाहर नहीं किया है क्योंकि उनके पूरी तरह से बाहर निकालने पर कोई व्यक्ति विधि का एक सम्पूर्ण विश्लेषणात्मक (analytical) स्वरूप बताने में समर्थ नहीं होगा।
यद्यपि सामाण्ड ने विषय की सीमा (boundary) को बड़े स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न किया है किन्तु वह एक ठीक और वैज्ञानिक परिभाषा देने में असफल रहा है। उसकी परिभाषा के आधार पर एक ही शब्द का बिल्कुल भिन्न प्रकृति की बातों का अर्थ देने के लिए प्रयोग हो सकता है और अनेक अस्पष्ट धारणाएं (vague notions) विषय के क्षेत्र में आ जायेंगी।
ग्रे- ये विधिशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार करता है कि यह विधि का विज्ञान है, अर्थात् न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों और उनमें अन्तर्निहित सिद्धान्तों को प्रणालीबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाना है। उसकी परिभाषा की बाद वाले विधिशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है। ग्रे की आलोचना करता हुआ जुलियस स्टोन कहता है कि अपनी परिभाषा में ग्रे विधिशास्त्र के किसी सीमा क्षेत्र को नियत करने में असफल रहा है बल्कि उसने विधिशास्त्र को घटा करके उसे केवल नियमों को क्रमबद्ध करने पर ला दिया है।
प्रो० एलेन- एक महान अंग्रेज विधिशास्त्री प्रो० एलेन ने विधिशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया है कि “यह विधि के आधारभूत सिद्धान्तों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह परिभाषा एक अमूर्त (abstract) परिभाषा प्रतीत हो सकती है परन्तु यह विषय की प्रकृति का सही रूप प्रस्तुत करती है। परिभाषा को विधि के केवल एक या कुछ पहलुओं पर सीमित करने से यह थोड़े समय में उपयोगिताहीन हो जायेगी।
एच० एल० ए० हार्ट- हार्ट प्रस्तुत शताब्दी के बड़े विधिशास्त्रियों में से है और उसने विधिशास्त्र के विकास में बहुमूल्य योगदान किया है। उसका सिद्धान्त आस्टिन के सिद्धान्त की कठोर विध्यात्मकता (positivism) के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। आस्टिन ने कहा था कि केवल समादेश (command) और अनुशास्ति (sanction) ही विधि के तत्व हैं। हार्ट के अनुसार विधि नियमों की एक प्रणाली है- प्राथमिक और गौण (secondary)-जिनका संयोग विधि की प्रकृति को सपष्ट करता है और विधिशास्त्र की कुंजी (key) प्रस्तुत करता है। प्राथमिक नियम कर्तव्य अधिरोपित करने वाले नियम हैं और गौण नियम वह शक्ति प्रदत्त करते हैं जो कर्तव्यों को निर्मित करने अथा बदलने का प्रावधान करत है। प्राथमिक नियमों का गौण नियमों द्वारा अनुपूरित किया जाना विधि पूर्व से विधि जगत की ओर कदम है। हार्ट की विधिक प्रणाली जो प्राथमिक तथा गौण नियमों का समामेलन है, प्राकृतिक विधि के न्यूनतम तत्व, अर्थात् विधि और नैतिकता, के बिना पूर्ण नहीं होगी। हार्ट ने विधि और नैतिकता को परस्पर सम्बन्धित करके, जिसे आस्टिन नहीं कर सका था, विधि के विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र के क्षितिज का विस्तार किया।
विधिशास्त्र की प्रमुख शाखाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
विश्लेषणात्मक विचारधारा- इस विचारधारा ने विधि के सम्बन्ध में एक नए युग का प्रारम्भ किया। उनके द्वारा दी गई विधि की परिभाषा स्पष्ट और सरल है। इसमें विधि की मान्यता का एक सरल उत्तर प्रस्तुत किया गया है।
इसने उन अनेक मिथ्या धारणाओं को समाप्त किया जिन्होंने विधि के वास्तविक अर्थ को अस्पष्ट और जटिल बना रखा था। इसके द्वारा विधि के बारे में अमूर्त और पूर्व निर्धारित धारणाओं को विधि की परिधि से बाहर निकाल दिया गया और अनेक भ्रमों का निवारण किया गया। विधि के क्षेत्र की एक सुस्पष्ट सीमा रेखा नियत हुई। इससे विधि के बारे में समुचित अध्ययन का विकास हुआ। अपनी सरलता, संगति तथा विवेचना की स्पष्टता के कारण इस सिद्धान्त का व्यापक प्रभाव हुआ। विश्लेषणात्मक सिद्धान्त ने विधि की पश्चात्वर्ती विचारधाराओं को आधार भूमि प्रदान किया। इसने आधुनिक काल में प्रारम्भ एवं प्रचलित अनेक विधिक विचारधाराओं के प्ररेणा स्रोत के रूप में काम किया है। सामण्ड और ग्रे ने विश्लेषणात्मक विध्यात्मक दृष्टिकोण में सुधार कर इसे आगे बढ़ाया। सामण्ड ने विधि निर्माता के रूप में संप्रभु की प्रमुखता को नहीं माना। उसके अनुसार विधि वे नियम हैं जिन्हें न्यायालय मान्य करता है और जिसके अनुसार कार्यवाही करते हैं। ग्रे विधि की परिभाषा इस रूप में करते हैं कि यह राज्य के न्यायिक अंग के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाया गया आचरण का नियम है। विधि में वैयक्तिक तत्व को महत्व देने के कारण बाद में विधि की यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। विधि का विशुद्ध सिद्धान्त, जिसका आगे विवेचन किया जाएगा, भी विश्लेषणात्मक आधार भूमि पर स्थित है।
ऐतिहासिक विचारधारा (Historical School) – ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक सैविग्नी को माना जाता है। सैविग्नी ने लोक चेतना (Volkgeist) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।
ऐतिहासिक विचारधारा अठारहवीं शताब्दी के “तर्कनावाद” और प्राकृतिक विधि सिद्धान्तों के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया के रूप में आई। यद्यपि ऐतिहासिक विचारधारा के भीतर आने वाले अनेक विशिष्ट विधिशास्त्री हैं और उनके विचारों एवं सिद्धान्तों में अन्तर भी है तथापि उनके चिन्तन में एक सामान्य बात भी है। वह यह है कि इस विचारधारा के चिन्तकों द्वारा यह कहा गया कि विधि लोगों की भाषा और आचार की भाँति अपना स्वरूप ग्रहण करती है और परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होती है। यह मत व्यक्त किया गया कि विधि एक क्रमिक और काषिक प्रक्रिया से विकसित होती है। विधि लोक जीवन से उत्पन्न होती है और उसकी भावना की अभिव्यक्ति है।
ऐतिहासिक विचारधारा ने एक सत्य को स्थापित किया कि किसी राष्ट्र की विधि प्रणाली पर लोगों की संस्कृति और चरित्र का बहुत प्रभाव होता है। यह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है।
ऐतिहासिक विचारधारा ने अनेक परवर्ती विधिशास्त्रियों को प्रभावित किया। इस विचार में कि विधि लोगों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है और क्रमशः विकसित होती है, भावी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के बीज निहित थे। इस विचारधारा द्वारा समाज और विधि के विकास के बीच एक कड़ी स्थापित की गई।
ऐतिहासिक विचारधारा ने इतिहास में जो रुचि उत्पन्न की उसने और आगे विधि सम्बन्धी शोध कार्यों को प्रेरणा दी। इतिहास के अध्ययन द्वारा अनेक विधिशास्त्रियों ने विधि के विकास के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और बाद में एक तुलनात्मक विधि विज्ञान की प्रणाली का आविर्भाव हुआ। इससे विधि में तुलनात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। तुलनात्मक प्रणाली से विभिन्न विधि प्रणालियों को एक दूसरे के निकट आने में सहायता मिली है। इससे प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि और लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की अनेक सम्भावनाएँ हैं।
समाजशास्त्रीय विचारधारा – सामाजशास्त्रीय विचारधारा में अनेक चिन्तन शामिल हैं जिनमें आपस में विभिन्नता है तथापि समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रियों के अध्ययन का मुख्य और सामान्य क्षेत्र विधि और समाज का एक दूसरे पर प्रभाव है। यह विचारधारा विधि को सामाजिक प्रगति में एक साधन के रूप में मानती है, इसलिए इसके अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है। विधि के निर्माण, इसके कार्यकरण और लागू किए जाने में जिन अनेकानेक बातों का प्रभाव पड़ता है वे सभी इसके अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। इस चिन्तन में समाज के लिए व्यक्ति और व्यक्तितत्व के लिए समाज के महत्व पर जोर दिया गया है।
यह कहा गया है कि विधि का अध्ययन समाज को सापेक्षता या सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। इस विचार का आधुनिक विधिक चिन्तन पर गहरा प्रभाव है। विधिशास्त्र के अध्ययन में उन तत्वों को क्रमशः उपयोगितापूर्ण ढंग से अपनाया गया है जिनको अपनाने का इस सिद्धान्त द्वारा आग्रह किया गया है। प्राकृतिक विधि के समर्थक तथा आदर्शवादी विधिशास्त्रियों ने भी अपनी विधि की परिभाषा और उकसी विषय-वस्तु को समाजशास्त्रीय चिन्तन के सन्दर्भ को एक नया रूप दिया है।
प्रश्न 3. विधि के आज्ञापक (Imperative) सिद्धान्त तथा इसी प्रकार के अन्य समान सिद्धान्तों की व्याख्या करें। इस कथन की समीक्षा करें कि यह सिद्धान्त अनुभव-सिद्ध न होकर युक्तिसंगत (Not Imperical but rational) है।
Discuss the imperative theory and the like theories. Critically examine the statement that this theory is not imperical but rational.
अथवा (OR)
“यह कहा जाता है कि ऑस्टिन का विधि का सिद्धान्त अनैतिक तथा अपूर्ण है।” इस कथन का मूल्यांकन करें।
It is said that Austine’s theory of law is immoral as well as incomplete. Evaluate this statement.
अथवा (OR)
ऑस्टिन की विधि की परिभाषा की त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। हार्ट अपनी विधि की परिभाषा में इन त्रुटियों को दूर करने में कहाँ तक सफल हुए हैं?
Mention the defects of Austin’s definition of law. How for Hart has been successful in removing these defects?
अथवा (OR)
विधि सम्प्रभु का आदेश (आज्ञा) है। ऑस्टिन के इस कथन की व्याख्या करें। भारतीय तथा आंग्ल व्यवस्था में इस सिद्धान्त के मूल्य का निर्धारण करें।
“Law is command of Sovereign”. Discuss this statement of Austin. Evaluate this theory of law in India as well as English set up.
ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक (Analytical) सिद्धान्त (शाखा) को समझाते हुए इस विचारधारा की प्रमुख कमियों का उल्लेख करें। इन कमियों को ऑस्टिन के समर्थकों ने किस प्रकार दूर किया है?
Explaining the Analytical (Theory) School of Austin. Evaluate the main shortcomings of this school (Thought). How for these shortcomings has been removed (explained) by supporters of Austine.
अथवा (OR)
विधिशास्त्र के क्षेत्र में एवं विधि के स्वरूप के निर्धारण में ऑस्टिन के योगदान की चर्चा करें।
Discuss the contribution of Austin in field of Jurisprudence and structure (Form) in determination of Law.
उत्तर- ऑस्टिन एक विज्ञान का विद्यार्थी था अतः इसके द्वारा विधि के परिप्रेक्ष्य (सन्दर्भ) में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना स्वाभाविक था। ऑस्टिन का मानना था कि विधि की परिकल्पना पहले से विद्यमान है तथा एक विधिशास्त्री का कार्य है उन विधिक परिकल्पनाओं का विश्लेषण करना। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक यौगिकों (Compounds) को, यौगिक (Compound) जैसा है वैसे ही उसका रासायनिक विश्लेषण करता है उसी प्रकार विधि की परिकल्पना जैसी अस्तित्व में है उसी का विश्लेषण विधिशास्त्री का कार्य है। जिस प्रकार एक रसायनशास्त्री रसायन कैसा होना चाहिए, इस पर विचार नहीं करता उसी प्रकार एक विधिशास्त्री को विधि कैसी होनी चाहिए (Ought to be), पर विचार नहीं करना चाहिए। एक विधिशास्त्री को विधिक परिकल्पनाओं के भविष्य या अतीत से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। एक विधिशास्त्री का प्रमुख कार्य अस्तित्वाधीन विधिक परिकल्पनाओं (legal concept) का विश्लेषण करना है। इसीलिए ऑस्टिन की विचारधारा को विश्लेषणात्मक विचारधारा (Analytical School) भी कहा जाता है। ऑस्टिन ने अपने इस विचार को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विधिशास्त्र की सीमा निर्धारित (The Province of Jurisprudence Determined) नामक पुस्तक में अभिव्यक्त की। यह पुस्तक 1832 में. प्रकाशित हुई।
ऑस्टिन की विचारधारा का समर्थन करने वालों का मानना है कि विधि का राज्य के साथ सम्बन्ध ही विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस विचारधारा के अनुसार विधि, राज्य द्वारा निर्गत आज्ञा या आदेश (Imperative or Command) है। राज्य के समर्थन के अभाव में विधि का अस्तित्व नहीं है। यदि राज्य विधि का प्रचर्तन सुनिश्चित नहीं करती तो विधि निरर्थक है। विधि के पालन के लिए राज्य द्वारा इसके उल्लंघन के लिए शास्ति या दण्ड (Sanction) निर्धारित किया जाना आवश्यक है। यदि विधि के अपालन या उल्लंघन के लिए शास्ति या दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है तो विधि का प्रवर्तन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसी कारण इस विचारधारा को आदेशात्मक (Imperative) विचारधारा भी कहा जाता है। यही कारण है कि विश्लेषणात्मक या आदेशात्मक विचारधारा के मानने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि न मानकर सकारात्मक नैतिकता (Positive Morality) मानते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय विधि जिन पर लागू होती है, वे स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्र होते हैं। इनके विरुद्ध किसी शास्ति (Penalty) को अधिरोपित कर पाना कठिन है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन आम बात है। यद्यपि हाल के वर्षों में अमेरिका की अगुआई में पश्चिमी देशों में सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों का सहारा लेकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या दण्डात्मक कार्यवाही का संचालन किया गया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कुछ सीमा तक सार्थकता का प्रवेश हुआ।
ऑस्टिन के समर्थकों के अनुसार विधिशास्त्रियों को विधि जैसी पायी जा रही है उससे ही सरोकार रखना चाहिए। इस विचारधारा के विधिशास्त्रियों के लिए विधि जैसी है (Law as it is) या सकारात्मक विधि (Past and Future) से सरोकार नहीं रखना चाहिए। विधि कैसी होनी चाहिए (Law as ought to be) या यह विधिशास्त्रियों के विचार की विषय- वस्तु नहीं है। यही कारण है कि इस विचारधारा को सकारात्मक विधि की विचारधारा (Positive School) भी कहा जाता है। इस विचारधारा का अधिक प्रभुत्व इंग्लैण्ड में है। इसे अंग्रेजी विचारधारा (English School) भी कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन लन्दन विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र पद (Chair) का प्रथम धारक था।
सकारात्मक विचारधारा या ऑस्टिनियन विचारधारा यह मानकर चलती है कि एक विकसित विधिक पद्धति (Developed legal system) का अस्तित्व है तथा विधिशास्त्रियों का कार्य इस विधिक पद्धति में विद्यमान मूलभूत (आधारभूत) परिकल्पनाओं (Basic) concepts) का तर्कपूर्ण विश्लेषण कर इनके मध्य सम्बन्धों को स्थापित करते हुए उनका वर्गीकरण करना है। इसलिए इस विचारधारा को विश्लेषणात्मक विचारधारा (Analytical school) भी कहा जाता है।
विश्लेषणात्मक विचारधारा एक ऐसी विधि व्यवस्था की परिकल्पना करती है जिसमें एक उच्चशक्ति होती है जो अधीनस्थ निकायों तथा अधीनस्थ लोगों के पालन हेतु आदेश (Command) या समादेश (imperative) या निर्णय करती है तथा अपने आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु शास्ति (Sanction) की व्यवस्था करती है। शास्ति का होना सम्प्रभु के आदेश के पालन की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है। ऑस्टिन की विचारधारा के मानने वालों के अनुसार सम्प्रभु या उच्चतर शक्ति की विद्यमानता के अभाव में विधि की कल्पना करना निरर्थक है। यही सम्प्रभु यां उच्चतर शक्ति विधि का प्रवर्तन या विधि का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है शास्ति के माध्यम से विधि का प्रवर्तन सुनिश्चित हो सकता है।
विश्लेषणात्मक या अधिरचनावादी (Imperative) विचारधारा की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं一
(1) विधि राज्य की उपज है तथा विधि का सम्बन्ध राज्य से है।
(2) सम्प्रभु के अभाव में विधि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सम्प्रभु तथा राजा का सम्बन्ध शक्ति तथा अधीनता का है। यह सम्बन्ध श्रेष्ठ तथा अवर का है।
(3) ऑस्टिन की विचारधारा के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं- समादेश (Command), कर्तव्य (Duty) तथा शास्ति (Sanction)।
(4) विधि सम्प्रभु का समादेश है। सम्प्रभु का तात्पर्य श्रेष्ठ शक्ति से है।
(5) विश्लेषणात्मक प्रथाओं को विधि नहीं मानती क्योंकि प्रथा को जब तक न्यायिक या सम्प्रभु की. सुरक्षा नहीं मिलती तब तक प्रथा विधि नहीं है।
(6) प्रोफेसर हार्ट के अनुसार विधि आदेश, अनुशास्ति तथा सम्प्रभु की त्रिवेणी है।
ऑस्टिन की विचारधारा के अनुसार विधि तथा नैतिकता पृथक् तत्व हैं। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र नैतिक दर्शन नहीं है। ऑस्टिन ने बेंथम के उस विचार को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार सम्प्रभु को विधि का उद्देश्य मानव प्रसन्नता का विकास है। ऑस्टिन के अनुसार बॅथम का उक्त सिद्धान्त नीतिशास्त्र का सिद्धान्त है।
ऑस्टिन के द्वारा लन्दन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान ‘दि प्राबिन्स ऑफ ज्युरिस्प्रूडेन्स डिटरमिण्ड’ शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए। ऑस्टिन ने अपने व्याख्यानों में विधि की प्रकृति और उसकी परिधि का वर्णन किया है। ऑस्टिन के अनुसार विधि सम्प्रभु का आदेश है। “Law is the Command of Sovereign” ऑस्टिन के मतानुसार विधि उचित या अनुचित पर आधारित न होकर सम्प्रभु शक्ति के आदेशों पर आधारित है। अतः ऑस्टिन का निश्चित मत है कि विधि का आधार प्रभुता सम्पन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित है। इसी को उन्होंने आदेशात्मक सिद्धान्त (Imperative theory) कहा है।
ऑस्टिन की विधि की परिभाषा में निम्नलिखित तीन तत्व आते हैं- आदेश, सम्प्रभु और अनुशास्ति ।
(1) आदेश (Command) – ‘आदेश’ राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या न करने के लिए आकांक्षा करे। आदेश सामान्य (General) या विशिष्ट (particular) दोनों प्रकार का हो सकता है। सामान्य आदेश वह है जो सभी व्यक्तियों पर सभी समयों पर समान रूप से लागू रहता है। जैसे-“Whoever commits murder will be hang” जो कोई भी कत्ल करेगा, उसे फाँसी दी जायेगी। विशिष्ट आदेश वह है जो कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सभी समयों के लिए अथवा सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समयों के लिए जारी किया जाय। सामान्य आदेश सकारात्मक विधि “Positive Law” के रूप में होता है और विशिष्ट आदेश ‘प्रशासी विधि’ के रूप में हो सकता है।
(2) सम्प्रभु (Sovereign)- ऑस्टिन ने विधि को सम्प्रभु का आदेश कहा है। ऑस्टिन ने सम्प्रभु शक्ति के दो आवश्यक लक्षण बताए हैं। प्रथम यह है कि सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, जिस पर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व न हो तथा द्वितीय यह है कि सम्प्रभु शक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रजा स्वेच्छा से उसकी आज्ञा पालन के लिए इच्छुक हो।
ऑस्टिन ने सम्प्रभु की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है-
“यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जिसका एक समाज श्रेष्ठ के आज्ञापालन का स्वभाव न हो, जिसका एक विहित समाज के अधिकांश भाग में स्वाभाविकतया आज्ञा पालन न होता हो तो वह निश्चित श्रेष्ठ उस समाज में सम्प्रभु होता है और समाज राजनीतिक एवं स्वतन्त्र समाज है।”
ऑस्टिन के द्वारा बताए गए दोनों ही लक्षणों को सम्प्रभु में होना चाहिए। इसमें से किसी एक के अभाव में वह सम्प्रभु नहीं हो सकता है।
(3) अनुशास्ति (Sanction) ऑस्टिन ने अपने आदेशात्मक सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया है कि सम्प्रभु के आदेश मात्र ही विधि का रूप धारण नहीं करते जब तक कि इनका उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था न हो, सही अर्थ में विधि नहीं करे जा सकते हैं। ऑस्टिन के अनुसार, आदेश के साथ अनुशास्ति के जुड़ा रहने पर ही इन आदेशों को सुस्पष्ट विधि कहा जा सकेगा।
ऑस्टिन की आलोचना – ऑस्टिन के विधि की उपर्युक्त परिभाषा की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं-
(1) ऑस्टिन का मत है कि ‘विधि सम्प्रभु का आदेश है’ यह बात ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा समर्थित नहीं है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ का आदेश नहीं वरन् रूढ़ियों मनुष्यों के आचरण को नियमित करती थीं। राज्य के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् भी रूढ़ियाँ आचरण को नियमित करती रही हैं। इस आधार पर रूढ़ियों को भी विधिशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए, किन्तु ऑस्टिन ने रूढ़ियों की उपेक्षा की है।
(2) वह विधियाँ जो अनुज्ञात्मक स्वरूप की होती हैं तथा सिर्फ विशेषाधिकार प्रदत्त करती हैं जैसे वसीयत अधिनियम जो वसीयती दस्तावेज के लेखन की रीति प्रतिपादित करता है, जिससे कि इसका विधिक प्रभाव हो सके, ऑस्टिन की विधि की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती हैं।
(3) संविधान के कन्वेन्शन जो अनिवार्य रूप से प्रवर्तित होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हुए भी ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार विधि नहीं कहलाते हैं। यद्यपि वे विधि हैं तथा विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं।
(4) ऑस्टिन के सिद्धान्त में न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित विधि के लिए कोई स्थान नहीं है जबकि अपने कार्य करने में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं।
(5) ऑस्टिन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सुस्पष्ट नैतिकता के अन्तर्गत रखा है। विधि का मुख्य तत्व अनुशास्ति है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अभाव है, किन्तु अव केवल यही इसे विधि कहे जाने से वंचित नहीं करेगा। आज के आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को भी विधि माना जाता है। अतः ऑस्टिन की की परिभाषा के अनुसार विधि की एक महत्वपूर्ण शाखा विधिशास्त्र के अध्ययन से अपवर्जित हो जायेगी।
(6) ऑस्टिन के मतानुसार यह मात्र अनुशास्ति ही है जो मनुष्य को विधि के पालन के लिए प्रेरित करती है। लॉर्ड ब्राइस ने इस बात की आलोचना की है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक ‘स्टडीज इन हिस्ट्री एण्ड ज्यूरिस्यूडेन्स’ में निश्चेष्टता, सहानुभूति, समादर, भय एवं तर्क को संक्षेप में उन हेतुओं के रूप में वर्णित किया है जो ‘किसी मनुष्य को विधि का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः ऑस्टिन की परिभाषा मान्य नहीं है।
(7) ब्राइस ने ऑस्टिन के विधि के सिद्धान्त की आलोचना की है तथा कहा है कि विधि को राज्य का आदेश मानने का अर्थ हुआ कि राज्य के सिवाय विधि का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है, परन्तु ऐतिहासिक आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि विधि का अस्तित्व उस समुदाय में भी था जब राज्य का उदय नहीं हुआ था। अतः ऑस्टिन के विधि सिद्धान्त का आधार संदेहास्पद है।
(8) विधि स्वेच्छापूर्ण आदेश नहीं है जैसी कि ऑस्टिन द्वारा कल्पना की गयी है, वरन् यह एक कायिक (Organic) प्रकृति का विकास है। डॉ० जे० ब्राउन ने कहा है कि “सर्वाधिक निरंकुश विधायक भी अपनी जाति एवं काल की भावना को जाने बिना न तो कोई बात सोच सकता है, न कोई कार्य करता है।” इसके अलावा विधि का विकास Blind Forces के अनुसार नहीं हुआ है, वरन् यह सोच समझ के साथ विकसित की गई है। इस प्रकार यह सदाचार सम्बन्धी एवं नैतिक तत्वों से पूर्णतः रहित नहीं है। ऑस्टिन ने विधि के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है।
(9) ड्यूगिट ने विधि को सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित करते हुए ऑस्टिन के सुस्पष्ट विधि सिद्धान्त को अमान्य कर दिया है। ड्यूगिट के मतानुसार सुस्पष्ट विधि जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ड्यूगिट ने समाज की आवश्यकताओं को ही विधि का मूल आधार माना है। उनके अनुसार विधि को राज्य की सम्प्रभु शक्ति पर आधारित करना उचित नहीं है, परन्तु डा० ऐलन के मतानुसार ‘ड्यूगिट ने राज्य की सम्प्रभु शक्ति की अवहेलना करके विधि के प्रति अत्यन्त संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है।
ऑस्टिन के सिद्धान्त का महत्व – यद्यपि ऑस्टिन के सिद्धान्त की बड़ी आलोचना हुई है और कहा गया है कि उन्होंने कानून और न्याय को अलग करके बड़ी भूल की लेकिन ऑस्टिन ने कानून और न्याय के बीच जो यह अन्तर स्थापित किया, यह प्राकृतिक विधि (Natural Law) के विरुद्ध बहुत बड़ी चुनौती थी। यह चुनौती आगे आने वाले विधिशास्त्र के सिद्धान्तों के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गयी। एकाघ सिद्धान्तों को छोड़कर सभी सिद्धान्तों ने – कानून और न्याय के मौलिक अन्तर को और बुनियादी एकता को स्वीकार किया।
ऑस्टिन ने ही यह बताया कि कानून की उत्पत्ति राज्य से होती है। प्रोफेसर ग्रे के – अनुसार ऑस्टिन महोदय इस योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं। उनका आदेशात्मक सिद्धान्त बाद के विधिशास्त्रियों के विचार का स्त्रोत बना। ग्रे ने ऑस्टिन के सिद्धान्त में कुछ सुधार किया। उन्होंने कहा कि राज्य का कानून ‘कानून’ नहीं ‘कानून का स्त्रोत’ है। इसके साथ अन्य भी स्रोत हैं जैसे रीतिरिवाज, पूर्वोक्ति आदि। ‘कानून’ वह स्रोत है जो कि राज्य की न्याय- शाखा के कार्य के नियम (Rules of Conduct) के रूप में घोषित किया गया है। सामण्ड भी इस संशोधन को मानते हैं। केल्सन (Kelson) की ‘वियना शाखा’ भी ऑस्टिन के सिद्धान्त से निकलती है।
विश्लेषणात्मक विचारधारा तथा भारतीय स्थिति- अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत में विधि-व्यवस्था प्रथागत थी। भारतीय विधि व्यवस्था प्रथागत धर्मशास्त्रों में निहित थी। सम्राट या राजा धर्म का प्रतीक था। राजा प्रजापालक तथा प्रजा का संरक्षक होता था। सम्राट या राजा ही विधि का तथा न्याय का प्रवर्तक माना जाता था। राजा धर्म को बनाए रखने के लिए या धर्म का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड (Penalty) की व्यवस्था करता था। धर्म से राजा तथा प्रजा दोनों बाध्य थे। भारतीय राजा भी विधि व्यवस्था के अधीन होने के कारण विधि के शासन (Rules of Law) का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाता था। ऑस्टिन के सम्राट या सम्प्रभु की भाँति भारतीय राजा विधि के शासन के ऊपर नहीं था।
भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य ने विदेशी शासन का सूत्रपात किया। अपने शासन व्यवस्था के दौरान ब्रिटिश शासकों ने हमेशा प्राचीन विधि-व्यवस्था का उपहास किया। ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑस्टिन की आदेशात्मक विचारधारा ही थी क्योंकि ऑस्टिन की विचारधारा पूर्ण अधिनायकवाद (dispositism) का समर्थन करती थी। इसलिए 1947 के पूर्व भारतीय विधिशास्त्रियों ने ऑस्टिन के आदेशात्मक विचारधारा का समर्थन करते हुए ऑस्टिन को अपना प्रभु या पिता माना। यह ऑस्टिन की अधिरचना वाली विचारधारा ही थी जिसके अन्तर्गत मैकाले तथा मेन अपनी ब्रिटिश विधि व्यवस्था को भारतीयों के ऊपर अधिरोपित कर सकते थे, क्योंकि ऑस्टिन की विचारधारा में विधि- व्यवस्था में नैतिकता या उचित अनुचित या आदर्श विधि पर विचार करने को स्थान नहीं दिया गया था। ब्रिटिश राज में विधि का उद्देश्य अंग्रेजों के हितों को पूरा करना था न कि प्रजा का कल्याण। प्रथम विधि आयोग (1834) के प्रथम अध्यक्ष मैकाले ने ब्रिटिश विधि पद्धति का भारतीय विधि पद्धति में समावेश करने में महत्वपूर्ण योगदान किया।
सन् 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात् भारतीय विधिक सिद्धान्त को नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ। स्वतन्त्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय संवैधानिक विधिशास्त्र का आधार बना। अब ऑस्टिन की विधि विचारधारा या आदेशात्मक विधि विचारधारा का अभियोजन करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। भारतीय संसद ने कमजोर तथा दबे- कुचले लोगों को उचित हिस्सा देने की विधायी आकांक्षा प्रकट की। भारतीय विधियों का उद्देश्य कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक सुधार बना।
शंकरी प्रसाद (1951) तथा सज्जन सिंह (1965) नामक दो वादों में उच्चतम न्यायालय ने विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत विधि का तात्पर्य सांविधानिक विधि है न कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद द्वारा संशोधन के माध्यम से अधिनियमित विधि। गोलक नाथ (1967) नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संवैधानिक संशोधन के अध्ययन से मौलिक विधि में संशोधन नहीं किया जा सकता।
गोपालन के वाद से ऑस्टिन की पुनर्वापसी- ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य, (1950) एस० सी० 27 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने विधायिनी द्वारा अधिनियमित विधि की सर्वोच्चता को प्रमुखता देते हुए नैतिकता तथा प्राकृतिक विधि के सिद्धान्तों की अनदेखी की। उच्चतम न्यायालय ने विधि की वैधता का निर्धारण करने से प्राकृतिक विधि के नियमों की भूमिका को अस्वीकार कर दिया। ऑस्टिन की विधि जैसी है (Law as it is) की विचारधारा को केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए० आई० आर० 1973 एस० सी० नामक वाद में भी अपनाया गया तथा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर एक सामान्य विधिक अधिकार माना तथा विधायिनी द्वारा अधिनियमित संशोधन को सामाजिक न्याय की अनदेखी करते हुए वैध माना। ए० डी० एम०, जबलपुर बनाम एस० शुक्ला, ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 1207 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निरोध के आदेश (order of detention) को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह विधि के शासन के नियम का उल्लंघन करता है। यद्यपि इस निर्णय को 44वें सांविधानिक संशोधन द्वारा निष्प्रभावी बना दिया गया है।
भारत में यद्यपि ऑस्टिन के अधिरचित विधि (Enacted Law) को प्रमुखता (सर्वोच्चता) प्रदान करने वाली विचारधारा को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक न्याय के आधार पर भारतीय संविधान के अन्तर्गत एकतरफ धकेल दिया गया था तथा विधि की वैधानिकता का परीक्षण सामाजिक न्याय तथा नैतिकता तथा समाज सुधार की कसौटी पर भी परखा जाने लगा। परन्तु उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण से यह प्रतिलक्षित होता है कि कभी-कभी ऑस्टिन की सकारात्मक विधि या अधिरचित विधि को सर्वोच्चता प्रदान करने वाली विचारधारा अपने प्रभाव दिखा देती है।
इंग्लैण्ड के प्रोफेसर हार्ट तथा हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लॉम फुलर का मानना था कि विधि से नैतिकता को पृथक् नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गाँधी के बाद में यह निर्णय दिया कि यदि विधायिका द्वारा अधिरचित विधि उचित (ऋजु Fair) न्यायोचित तथा नैतिक नहीं है तो ऐसी विधि असंवैधानिक होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि मेनका गाँधी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस विचारधारा को सही माना कि यह भी देखा जाना चाहिए कि विधि कैसी होनी चाहिए (What law ought to be) विधि को नैतिकता, न्याय तथा विधि के शासन एवं प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर भी खरी उतरनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने विधि की एक मात्र कसौटी कि यह विधायिनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा अधिरचित होनी चाहिए, को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व ऑस्टिन की विचारधारा अंग्रेजों के हित साधन का माध्यम थी। अतः इस विचारधारा को प्रमुखता प्राप्त थी, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत कल्याणकारी राष्ट्र बना तथा जनता का हित विधि का उद्देश्य बना तथा विधि की संवैधानिकता या वैधता सामाजिक न्याय, नैतिकता तथा उचितता की कसौटी पर परखी जाने लगी तथा ऑस्टिन के सकारात्मक, आज्ञापक विचारधारा का प्रभाव भारत में कम हुआ।
प्रश्न 4. सामण्ड की विधि की परिभाषा दीजिए। यह परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा की कमियों को दूर करने में कहाँ तक सफल हुई है?
Give Salmond’s definition of law. How far Salmond’s definition has been successful in removing defects of Austin’s definition?
अथवा (OR)
सामण्ड द्वारा दी गयी विधि की परिभाषा का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।
Critically examine (evaluate) the definition of law as given by Salmond.
अथवा (OR)
सामण्ड तथा ऑस्टिन की विधि की परिभाषा की तुलना कीजिए। इन दोनों परिभाषाओं में से कौन-सी परिभाषा आपके विचार में अधिक उपयुक्त है?
Compare the stin’s and Salmond’s definition of Law. Which definition is comparatively better according to your opinion?
अथवा (OR)
सामण्ड की विधि की परिभाषा को समझाइए। क्या यह ऑस्टिन की परिभाषा को सुधारती है?
Explain Salmond’s definition of Law. Does it amend Austin’s definition of Law?
उत्तर- सामण्ड ने विधि की परिभाषा इस प्रकार दी है-
“Law is the body of principles recognised and applied by the ‘State in the administration of justice. In other words, the law consists of the rules recognised and acted on by Court of Justice.”
विधि राज्य द्वारा, न्याय प्रशासन में मान्यता प्राप्त एवं प्रयुक्त सिद्धान्तों का एक समूह है। दूसरे शब्दों में, विधि उन नियमों का समूह है जो न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिसे न्यायालय उपयोग में लाती है।”
यह परिभाषा दो बातों पर जोर देती है-
(1) न्यायालयों पर अधिक जोर- सामण्ड के अनुसार, विधि की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें न्यायालय के पास जाना चाहिए, न कि सम्प्रभु के पास। न्यायालय के पास आज्ञा पालन करवाने की शक्ति होती है, न कि सम्प्रभु के आदेश में। सामण्ड महोदय ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना करते हैं कि विधि सम्प्रभु के आदेश पर निर्भर होती है, क्योंकि सभी विधियाँ सम्प्रभु का आदेश नहीं होतीं और न ही विधानमण्डल द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। पूर्वोक्तियाँ (Precedents), रूढ़ियाँ (Customs) एवं साम्या (Equity) भी विधि का भाग एवं स्रोत हैं। सामण्ड महोदय का कथन है कि विधि न्यायालय द्वारा मान्य नियमों को कहते हैं, इसलिए सभी विधियाँ चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, न्यायालय द्वारा चलायी जाती हैं। न्यायालय उन नियमों को नहीं मानता जो विधिमान्य न हों। कोई भी नियम जो सुचारु रूप से उपयोग में (in practice) नहीं लाये जाते, विधि नहीं कहे जा सकते, यह न्यायालय पर निर्भर है कि नियम को विधि माने।
(2) विधि का उद्देश्य- ऑस्टिन द्वारा अस्वीकार किये गये विधि के उद्देश्य को सामण्ड महोदय ने पूरा किया तथा कहा कि न्याय ही विधि है इसे विधि को न्याय देना भी कहा जा सकता है। वे फिर कहते हैं कि विधि के नियम एक दृष्टि से राजा के आदेश हैं जो राजा द्वारा जनता पर लागू किए जाते हैं तो दूसरी दृष्टि से वे उचित और अनुचित के सिद्धान्तों के समूह भी हैं जो राज्य के महत्वपूर्ण अंग न्यायालय द्वारा चलाये जाते हैं। न्यायालय के कामों के लिए विधि केवल अधिकार (right) या शक्ति ही नहीं है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। राज्य की यह वाणी जनता के समक्ष निकली हुई न्याय की आवाज है।
सामण्ड की परिभाषा की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परम्परागत संविधान एवं संविधान के बीच एक रेखा खींच देती है। परम्परागत विधि न्यायालयों में नहीं चल सकती, जबकि संवैधानिक विधि को न्यायालयों में चलाया जा सकता है।
सामण्ड महोदय की परिभाषा प्रो० ग्रे से काफी मिलती-जुलती है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार- राज्य का कानून या किसी सुव्यवस्थित समाज का कानून महज संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है तथा न्यायालय उन्हें अमल में लाते हैं।
आलोचना – सामण्ड की विधि की परिभाषा की आलोचना इस प्रकार की जा सकती है-
(1) सामण्ड महोदय कहते हैं कि विधि वे नियम समूह हैं, जिन्हें न्यायालय एवं न्याय प्रशासन में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार गणित शास्त्र का यह नियम है कि दो +दो = चार होते हैं, तो विधि मानी जायेगी, क्योंकि न्यायालय न्याय- प्रशासन में इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, वरन् वे इसको मान्यता प्रदान करते हैं, किन्तु यह नियम विधि का भाग नहीं है।
(2) विधि तभी विधि कहलायेगी जब न्यायालय द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हुई हो। यदि इस परिभाषा को ठीक मान लिया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा प्रशासकीय विधि को कभी विधि कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार केवल वास्तविक विधि सिविल विधि को ही कहा जा सकेगा, अन्य विधियाँ नहीं।
(3) न्यायाधीश का एकमात्र उद्देश्य होता है विधि को अमल में लाना। यदि हम विधि की परिभाषा का प्रारम्भ न्यायाधीशों के कार्यों से करते हैं तो इस प्रकार की परिभाषा ठीक ‘मोटर कार’ की एक परिभाषा के समान होगी जिसमें यह कहा गया है कि ‘मोटर कार’ वह गाड़ी है जिसे ड्राइवर चलाता है। यह परिभाषा अपने में पूर्ण नहीं है। न्यायालय तो कानून रूपी मोटर का ड्राइवर है।
(4) न्याय-प्रशासन का अर्थ होता है कि विधि को ठीक प्रकार से लागू करना। यदि न्याय प्रशासन की विधि को लागू करने के रूप में परिभाषा दी जाती है तो विधि की परिभाषा इस प्रकार से करना कि विधि वह है जो कि न्याय प्रशासन में लागू की जाती है, ठीक नहीं लगता है। विधि की परिभाषा को न्यायालय के कार्यों में ढूँढने पर अब तो यही होता है कि हम उसी प्रश्न को खोजने निकल पड़े, जिस प्रश्न के उत्तर को हम खोजने निकले थे।
(5) न्याय प्रशासन के रूप में कानून की परिभाषा करके सामण्ड महोदय ने परिभाषा के तार्किक क्रम को पलट दिया है। कानून का निर्माण पहले आता है, कानून का प्रशासन बाद में। न्यायालय द्वारा लागू होने के पहले कानून का बनना जरूरी होता है। सामण्ड की परिभाषा में कमी यह है कि वह इस बात की पहले से ही कल्पना कर लेता है कि कानून तर्क की दृष्टि में न्याय प्रशासन के पश्चात् आता है। सामण्ड की परिभाषा को सूक्ष्म रूप से देखने पर यह ज्ञात होता है कि सामण्ड के अनुसार कोई भी नियम इस कारण विधि है, क्योंकि न्यायालय उसे अमल में लाया है और लागू किया है, क्योंकि यह एक विधि है।
(6) सामण्ड ने विधि की परिभाषा इस प्रकार देकर उस वस्तु को ही समाप्त कर दिया है, जिसे परिभाषित करने के लिए वे उद्यत हुए थे। सामण्ड महोदय कहते हैं कि संहिता का अधिनियम आदि विधि नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश इनमें वर्णित विधि का इनके शाब्दिक अर्थों से भिन्न कोई दूसरा अर्थ लगा सकता है यदि ऐसी बात है तो हम पूर्वोक्तियों को क्यों विधि मानें? पूर्वोक्तियाँ भी पश्चात्वर्ती न्यायालय द्वारा अन्यथा की जा सकती हैं अतएव पूर्व निर्णय विधि नहीं है।
(7) सामण्ड महोदय नै न्याय को ही विधि का उद्देश्य माना है। पैटन महोदय इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि केवल न्याय को ही विधि का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। विधि कई उद्देश्यों को पूरा करती है। विधि का मुख्य उद्देश्य देश में शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना है।
इन सब आलोचनाओं के होते हुए भी सामण्ड महोदय के योगदान को सराहनीय कहा जा सकता है। इन्होंने ऑस्टिन की बहुत सी कमियों को दूर किया है। ऑस्टिन के कथनानुसार-कानून का एकमात्र स्रोत राज्य है। उन्होंने प्रथा आदि को कानून के क्षेत्र से बाहर करके अन्तर्राष्ट्रीय विधि को भी विधि के क्षेत्र से निकाल दिया था। उनकी कानून की परिभाषा हिन्दू-विधि के साथ ही ठीक नहीं बैठती थी। सामण्ड ने इस कमी को दूर किया। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन के ‘आदेश और भय’ के शब्द कानून के सूखे पक्ष की ओर ही इशारा करते थे। मनुष्य भय से ही कानून का पालन नहीं करता वह कानून का पालन इस कारण करता है कि वह न्याय की समूची अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय विधि को लागू ही नहीं करती, बल्कि उसको बनाती भी है। यह बात एकदम सत्य है। ऑस्टिन राज्य की विधायिनी को महत्व देते हैं किन्तु सामण्ड साथ में न्यायालय को भी महत्व देते हैं। उनके अनुसार दोनों में न्यायालय का महत्व अधिक है।
सामण्ड महोदय की परिभाषा तार्किक ढंग से भी सही है, क्योंकि इसे सीधे तथा उलटे. दोनों ढंग से पढ़ा जा सकता है। समस्त कानून न्यायालय द्वारा मान्य होते हैं और कोई भी नियम जो न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होते, वे विधि के नियम नहीं होते हैं।
प्रश्न 5. (i) केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धान्त का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate the pure theory of law of Kelson.
अथवा (OR)
केल्सन के विधि का विशुद्ध सिद्धान्त लिखिए। केल्सन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मूल सन्नियम (Grund Norm) क्या हैं?
Write down the Kelson’s pure theory of Law. What are ‘Grund Norm’ of International law according to Kelson.
(ii) केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धान्त मानवीय तत्व की उपेक्षा करता है। इस सम्बन्ध में इस कथन की समीक्षा कीजिए।
Kelson’s Pure theory of Law lacks Human element” Criticise this statement in this regard.
अथवा (OR)
हेन्स केल्सन द्वारा प्रतिपादित विधि के विशुद्ध सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर (i)- हेनरी केल्सन वियेना विश्वविद्यालय में सन् 1911 में विधि का प्रोफेसर था। हेनरी केल्सन ने सन् 1934 में लॉ क्वार्टली रिव्यू (Law Quarterly Review) में एक निबन्ध लिखा जिसका शीर्षक था विधि का विशुद्ध सिद्धान्त (Pure Theory of Law)। इस निवन्ध के माध्यम से केल्सन ने एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो ऑस्टिन के सिद्धान्त का संशोधित रूप था। सन् 1945 में केल्सन ने इस सिद्धान्त का और अधिक विस्तार अपने निबन्ध विधि तथा राज्य के सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Law and State) नामक निबन्ध के माध्यम से किया।
हेनरी केल्सन विधिशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानता था। केल्सन के अनुसार विधिशास्त्र, मानकीय विज्ञान (Normative Science) या नियमों का विज्ञान (Science of Rules) है। विधिशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान से पृथक् विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कारण तथा प्रभाव के क्रमबद्धता का प्रतिवेदन (Natural science or statement of sequence of cause and effect)। यदि आक्सीजन तथा हाड्रोजन एक तथा दो के अनुपात में मिलते हैं तो इसकी परिणति (प्रभाव) पानी या जल के निर्माण में होती है। प्राकृतिक विधि या भौतिक विधि में व्यतिक्रम पर कम प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भौतिक विज्ञान में एक मात्र व्यतिक्रम भौतिक नियम को अवैध बना देगा। विधिशास्त्र में कारण प्रभाव का सम्बन्ध नहीं होता। भौतिक नियम के अन्तर्गत सभी परिस्थितियों में एक ही प्रभाव होता है। परन्तु विधि के विज्ञान के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता। विधिशास्त्र या विधि विज्ञान में मानकों का सम्बन्ध या मानकीय सम्बन्ध (Normative Connection) का अस्तित्व होता है। यदि एक मानक का अस्तित्व है तो दूसरे का अस्तित्व होना चाहिए। उदाहरण के रूप में विधिशास्त्र के मानक के अनुसार यदि अ हत्या करता है तो वह मृत्युदण्ड से दण्डित होगा। विधि जब विधि का उल्लंघन होता है तब तथा जब उसके परिणाम घटित नहीं होते दोनों परिस्थितियों में वैध होती है अर्थात् यदि अ हत्या नहीं करता तब भी हत्या का परिणाम मृत्युदण्ड होगा। यदि अ की हत्या नहीं होती तब भी हत्या के लिए मृत्युदण्ड की सजा का नियम यथावत बना रहेगा। यदि विधि का उल्लंघन होता तब या जब विधि का उल्लंघन नहीं होता तब भी विधि (Law) की वैधता बनी रहती है जब कि भौतिक नियम या मानक कारण तथा प्रभाव के अन्तर्गत प्रभावी होते हैं।
केल्सन के अनुसार राज्य तथा विधिक व्यवस्था एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। केल्सन कहता है कि विधि को अन्य विज्ञान से पृथक् तथा शुद्ध रखना चाहिए। केल्सन के विधि के शुद्ध विज्ञान के सिद्धान्त की प्रमुख समस्या यह है कि ये मानक या नियम (Norms) कहाँ से प्राप्त होते हैं। इन मानकों की विधिकता के परीक्षण का आधार क्या है।
केल्सन के अनुसार विधिशास्त्र, मानकों या नियमों का विज्ञान है। इन मानकों की वैधता की कसौटी के रूप में केल्सन मूल नियमों या मौलिक मानकों (Grund Norms or Fundamental Norms) को देखता है। केल्सन के अनुसार सभी मानक (Norms) या नियमों की वैधता को मौलिक मानक की कसौटी पर परीक्षित करना चाहिए। यदि कोई मानक (Norms) या नियम मूल मानक या मौलिक नियम की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता तो वह मानक (Norm) वैध मानक न होकर अवैध मानक या अवैध नियम होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि मूल मानक या मौलिक नियम का पता कैसे लगाया जाय। किसी विधि व्यवस्था में मूल मानक या मौलिक नियम (Grund Norm) को सुनिश्चित करना कठिन है। मौलिक मानक का व्यकलन (Deduction of Grund Norm) विधि विज्ञान के किसी भी शुद्ध सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। यह प्रारम्भिक परिकल्पना का तार्किक सबूत नहीं दिया जा सकता। इंग्लैण्ड के लिए संसद के माध्यम से जिस विधि का निर्माण सम्राट करता है वह मौलिक मानक है तथा इंग्लैण्ड के विधिक मानक इस मौलिक मानक की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। हम ऐतिहासिक रूप से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस सिद्धान्त को इंग्लैण्ड में कैसे स्वीकार किया गया। परन्तु हम उसे शुद्ध तर्कों द्वारा प्रदर्शित या साबित नहीं कर सकते। इन मौलिक मानकों, नियमों का प्राथमिक उद्देश्य है कि यह राज्य में कुछ व्यक्तियों को मानकों के निर्माण की क्षमता प्रदान करता है जो मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया का प्रतिपादन करें। इसी आधारभूत या मौलिक मानक से मानक निर्माण की शक्ति निचले स्तर पर प्रवाहित होती है जो एक स्तर (Stage) से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होती है। प्रत्येक स्तर पर निर्मित मानकों की वैधता की परख मौलिक मानक की कसौटी पर ही होगी। विधि निर्माण या मानक निर्माण के विभिन्न स्तर संयुक्त रूप से किसी राष्ट्र की विधिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मानकीय विज्ञान का यह सिद्धान्त सार्वभौमिक है तथा किसी भी विधिक व्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है। चूंकि यह सिद्धान्त एक विशिष्ट विधिक व्यवस्था के लिए सीमित न होकर सभी विधिक व्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है अतः केल्सन अपने इस सिद्धान्त को विधि का विशुद्ध सिद्धान्त (Pure theory of law) कहता है। केल्सन अपने सिद्धान्त को विशुद्ध विधि का सिद्धान्त इसलिए भी कहता है कि इसके मानकीय विज्ञान (Normatic Science) का सम्बन्ध सिर्फ विधिक व्यवस्था तक ही सीमित है। इसका समाज तथा अन्य परा भौतिक व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः यह शुद्ध (Pure) है। केल्सन के अनुसार विधिक विज्ञान (Legal Science) का अन्य विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है। विधि की वैधता, विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही निर्धारित करनी चाहिए। इसका समाज की अन्य व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। विधि की वैधता का परीक्षण विधिक आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसे अन्य आधार से पृथक् रखते हुए शुद्ध रखना चाहिए। विधि की वैधता का सम्बन्ध सामाजिक तथ्य या न्याय के उच्च सिद्धान्तों से नहीं है यह विशुद्ध रूप से विधिक व्यवस्था के मौलिक मानकों के आधार पर परीक्षित होनी चाहिए। इसीलिए केल्सन अपने सिद्धान्त को विधि का विशुद्ध सिद्धान्त (Pure theory of law) कहता है। केल्सन, विधि के साथ इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान तथा नैतिकता को मिलाने के विरुद्ध है क्योंकि ये शास्त्र विधिशास्त्र को अशुद्ध करते हैं। विधि को शुद्ध रखने के लिए उसे उपरोक्त अशुद्धियों से मुक्त रखना चाहिए।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि केल्सन विधिशास्त्र को मानकों या नियमों का विज्ञान मानता है। वह विधिशास्त्र को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र तथा नैतिकता से मिश्रित कर विधि को अशुद्ध नहीं करना चाहता। केल्सन के अनुसार विधि एक मानक या नियम (Norm) है जिसमें शास्ति विद्यमान होती है। मानक या नियम या विधि एक प्रकार का निदेश है जिसके अन्तर्गत एक कार्य अनुज्ञात, अधिकृत या समादेशित होता है। केल्सन के स्वयं के शब्दों में मानक (Norm) या विधि का तात्पर्य है कुछ होना चाहिए, कुछ अवश्य घटित होना चाहिए विशेषकर यह कि मानकों को एक विशिष्ट बर्ताव या आचरण करना चाहिए। यदि ऐसा मानव या मनुष्य नहीं करेगा तो विधि विरुद्ध होगा। विधि या मानक (Norm) मनुष्यों को विशिष्ट आचरण समादेशित करती है इस प्रकार विधि समादेश है जिसके द्वारा कोई कार्य अनुज्ञांत (Permitted) होता है या कुछ आचरण प्रतिबन्धित होता है।
केल्सन के अनुसार विधि व्यवस्था (Legal order) मानकों का अधिक्रम (Hierarchy) है तथा विधिशास्त्र इन मानकों का ज्ञान या जानकारी है जो किसी विधि व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये मानक किसी उच्चतर स्रोत से अवतरित होते हैं, प्राप्त होते हैं विधिक मानक ऊपर से नीचे तक तथा नीचे से ऊपर तक व्यवस्थित मानकों की श्रृंखला है जो मौलिक मानक (Grund Norm) से नीचे की तरफ आती है। नीचे वाले मानक उच्चतर मौलिक मानक से वैधता प्राप्त करते हैं। मौलिक मानक (Fundamental Norms) अन्य मानकों (Other Norms) को वैधता तथा प्राधिकार प्रदान करते हैं। मानकों के इस पिरामिड का आधार मूल मानक (Grund Norm) है। विधि सिद्धान्त (Legal theory) का प्रमुख कार्य मौलिक मानक तथा अन्य मानकों के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट करना है। केल्सन के सिद्धान्त की प्रमुख समस्या मौलिक मानक के आधार की तलाश करना है। मौलिक मानक (Grund Norm) का स्रोत क्या है, इसकी वैधता की कसौटी क्या होगी। यही केल्सन के सिद्धान्त की प्रमुख समस्या है। मानकों की श्रृंखला की सबसे ऊपरी (सर्वोच्च) कड़ी का पता लगाना ही केल्सन के सिद्धान्त की समस्या है विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सर्वोच्च मानक या मौलिक मानक (Superior Norm or Grund Norm) को सुनिश्चित करना कठिन है। केल्सन मौलिक मानक को विधि से परे मानते हैं। यह उनकी विधि को शुद्ध रखने के सिद्धान्त को निरर्थक कर देता है क्योंकि मौलिक मानक विधि व्यवस्था से परे होता है। वही सभी मानकों को वैधता प्रदान करता है। भारत में भारतीय संविधान मौलिक मानक (Grund Norm) है तथा सभी अन्य मानक इसी से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं तथा संविधान को संवैधानिक सभा के प्रस्ताव से वैधता प्राप्त होती है। संवैधानिक सभा के प्रस्तावों को लोकमत से वैधता प्राप्त होती है परन्तु उससे ऊपर मौलिक मानक का पता लगाना कठिन है।
केल्सन तथा ऑस्टिन (Kelson and Austine) – ऑस्टिन राज्य तथा विधि के मध्य द्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। ऑस्टिन के अनुसार राज्य या सम्राट तथा विधि का अस्तित्व पृथक् है। विधि, सम्राट या राज्य के अधीनस्थ होती है। विधि सम्राट से उत्पन्न होती है अतः विधि सम्राट को नियन्त्रित नहीं कर सकती। केल्सन के अनुसार राज्य विधि व्यवस्था की एकता का प्रतीक है। राज्य विधि व्यवस्था की पर्यायवाची है अर्थात् केल्सन सम्राट तथा विधि व्यवस्था में अन्तर को स्वीकार नहीं करते। अतः केल्सन के अनुसार राज्य तथा विधि में अन्तर नहीं है।
ऑस्टिन के अनुसार राज्य विधि का सृजन करता है, विधि राज्य को नियन्त्रित नहीं करती जबकि केल्सन के विचार में राज्य विधि द्वारा नियन्त्रित होता है। इस प्रकार केल्सन, ऑस्टिन को संशोधित करता है।
ऑस्टिन का आज्ञापक सिद्धान्त यह कहता है कि विधि सम्राट का समादेश (Command) है। केल्सन यद्यपि विधि के अन्तर्गत शास्ति (Sanction) को आवश्यक समझते हैं परन्तु केल्सन के लिए विधि सम्राट् का व्यक्तिगत समावेश नहीं है। विधि एक ऐसा परिकल्पनात्मक निर्णय है जिसके अन्तर्गत विहित आचरण का पालन करने पर व्यक्ति शास्ति (Penalty) आमन्त्रित करता है। इस प्रकार केल्सन का सिद्धान्त ऑस्टिन का संशोधित स्वरूप है। ऑस्टिन का विश्लेषणात्मक सिद्धान्त लोकविधि (Public law) तथा निजी विधि (Private Law) में अन्तर करता है। इसके अनुसार लोकविधि सम्राट् या राज्य के अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य तथा अधिकार का निरूपण करती है जबकि निजी विधि सामान्य जनता (प्रजा) के आपसी कर्तव्य तथा अधिकारों से सम्बन्धित होती है। केल्सन के अनुसार लोकविधि तथा निजी विधि के मध्य यह अन्तर निरर्थक है। यदि सम्राट या राज्य को पृथक् इकाई न माना जाय तो लोकविधि तथा निजी विधि में कोई अन्तर नहीं होगा। चूँकि संविदा विधि जैसे निजी विधि भी अपनी वैधता मौलिक मानक (विधि) (Grund Norm) से प्राप्त करती है जिससे लोकविधि वैधता प्राप्त करती है अतः लोकविधि तथा निजी विधि के मध्य अन्तर निरर्थक है।
ऑस्टिन अन्तर्राष्ट्रीय विधि को कठोर अर्थों में विधि नहीं मानता क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्प्रभु राष्ट्रों को बाध्य करती है जबकि ऑस्टिन के अनुसार सम्राट या सम्प्रभु विधि से बाध्य नहीं हैं। विधि सम्राट की कृति (Creation) मात्र है। केल्सन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विधिक व्यवस्था (जिसे अन्यथा राज्य कहा जाता है) से ऊपर है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मानक या नियम (Norms) राष्ट्रों पर बाध्यकारी होते हैं। केल्सन के राज्य की सम्प्रभुता की उस अस्वीकृति ने ऑस्टिन के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में विद्यमान कठिनाई को दूर किया। इस प्रकार केल्सन, ऑस्टिन का संशोधित रूप है।
ऑस्टिन के सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रथा को विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि प्रथा सम्प्रभु की कृति नहीं है। केल्सन प्रथा को विधि की परिकल्पना के अन्तर्गत स्थान देता है क्योंकि इसके लिए एक मध्यवर्ती मानक की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत लोकप्रिय व्यवहार (प्रथा) विधिक मानक का सृजन कर सके।
इस प्रकार स्पष्ट है कि केल्सन का सिद्धान्त ऑस्टिन के सिद्धान्त पर संशोधित या सुधार या अभिवृद्धि (Improvement) है। केल्सन ने ऑस्टिनवादियों की कई कमियों तथा परेशानियों को दूर किया। यद्यपि केल्सन के सिद्धान्त की कुछ सीमाएँ हैं। राज्य तथा विधिक व्यवस्था की एकरूपता ने कई प्रश्नों को जन्म दिया। राज्य को कभी-कभी विधि-व्यवस्था के बाहर जाकर कार्य करना पड़ता है। केल्सन के अनुसार यदि प्रत्येक राष्ट्र का मौलिक मानक (Ground Norm) उसके लोक आचार के अनुसार पृथक् होता है तो केल्सन का सामान्य विधिशास्त्र (Jurisprudentia Generalis) की परिकल्पना निरर्थक हो जाती है।
केल्सन के अध्यापक लाउटर पाच (Lauter Patch) ने अपने शिष्य की आलोचना इस आधार पर की कि वह राष्ट्रीय विधि पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्राथमिकता को स्वीकार करता है अतः केल्सन प्राकृतिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश देता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वैधता या विधिकता (Lawness) मौलिक मानक (Grund Norm) से प्राप्त नहीं हो सकती। केल्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वैधता मौलिक भानक की कसौटी पर परीक्षण के बिना स्वीकार की है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि केल्सन के विधि के शुद्ध सिद्धान्त या मानकीय विज्ञान के सिद्धान्त की वास्तविक कमजोरी है।
उत्तर (ii)- केल्सन के विधि सम्बन्धी विशुद्ध सिद्धान्त की आलोचना – केल्सन द्वारा प्रतिपादित विधि के विशुद्ध सिद्धान्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधि के अन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं क्योंकि वे विधिक कर्तव्यों को ही विधि का सार मानते हैं। वे विधिक अधिकार को उस व्यक्ति का जो कि उसकी पूर्ति की उपेक्षा करता है केवल कर्तव्य मात्र निरूपित करते हैं। यह बात आपराधिक विधि के सन्दर्भ में अधिक स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है जहाँ व्यवस्थित व्यक्ति का कोई विधिक अधिकार नहीं होता वरन् राज्य स्वयं ही अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करता है तथापि केल्सन के विधि सम्बन्धी विशुद्ध सिद्धान्त की अनेक विधिशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है-
(1) केल्सन द्वारा प्रतिपादित विधि का विशुद्ध सिद्धान्त वस्तुतः विधिशास्त्र की महाद्वीपीय शाखा और न्याय के सिद्धान्तों के बीच समन्वय स्थापित करने का एक प्रयास है। इसे विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी (Analytical Positivism) की चरम सीमा का प्रतीक भी कहा जा सकता है। इस सिद्धान्त ने ऑस्टिनवादी विचारकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल कर दिया तथापि इस सिद्धान्त की अपनी सीमाएँ भी हैं। केल्सन के विधि सम्बन्धी विशुद्ध-सिद्धान्त में मूल मानक एक ऐसी परिकल्पना है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि मूल- मानक प्रत्येक देश की प्राचीन परम्पराओं और इतिहास के अनुसार अलग-अलग हो सकता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य विधिशास्त्र के सिद्धान्त को त्याग देना होगा। परन्तु ऐसा कदापि उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त केल्सन के सिद्धान्त ने राज्य और विधि की वैधता को समाप्त करके राज्य की शक्ति को अत्यधिक सीमित कर दिया है, जो उचित नहीं है। अनेक अवसरों पर राज्य को विधिक क्रम के दायरे से बाहर भी कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ मिलकर कार्य करना होता है और ऐसे कार्यों का क्षेत्र विधिक क्रम के बाहर भी हो सकता है। इसी प्रकार केल्सन ने अपने विधि – सिद्धान्त द्वारा पब्लिक और प्राइवेट विधि के अन्तर को साबित करके राज्य के विधिक दायित्व के निर्धारण की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया। किसी कल्याणकारी राज्य में राज्य के प्राधिकारियों की अधिकार शक्ति के निर्धारण के लिए लोक विधि और प्राइवेट विधि में विभेद होना आवश्यक है।
(2) केल्सन के विद्यार्थी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ प्रो० वाटरपाँच ने विशुद्ध विधि-सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधि पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता देकर केल्सन ने प्राकृतिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश देने का रास्ता खोल दिया है। उनके विचार से अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वैधता किसी भी मूल-मानक पर आधारित नहीं है, फिर भी केल्सन ने इसे राष्ट्रीय विधि की बजाय गुरुतर माना है। लाटरपाँच ने केल्सन की इस धारणा को उनके विशुद्ध विधि-सिद्धान्त का महान् दोष माना है। लाटरपांच की इस आलोचना का प्रो० ज्यूलिस स्टोन ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘द प्रॉविन्स एण्ड फंक्शन ऑफ लॉ’ में उत्तर देने का प्रयास किया है। प्रो० स्टोन का कहना है कि केल्सन की मूल- मानक की धारणा एक ऐसी परिकल्पना है जिसकी अवधारणा विधि के विशुद्ध विज्ञान द्वारा नहीं की जा सकती। इसे तो विधि के क्षेत्र के बाहर से ही चुनना होगा तथा बिना सबूत के इसे मूल मानक के अंश रूप में मानना पड़ेगा। परन्तु निवेदित है कि प्रो० स्टोन का यह तर्क केवल इस ओर संकेत करता है कि इस विधि के विशुद्ध विज्ञान का क्षेत्र सीमित है परन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वैधता को स्थापित नहीं करता है।
(3) लास्की ने केल्सन के विशुद्ध सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा कि यह व्यर्थ की दिमागी कसरत है जिसका वास्तविक जीवन में कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। कुछ विधि-वेत्ताओं ने केल्सन को कल्पना-लोक में विचरने वाला तर्कशास्त्री निरूपित किया है।
(4) फ्रीडमैन के अनुसार केल्सन का विधि-सम्बन्धी विशुद्ध सिद्धाना आधुनिक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से पर्याप्पा है। आधुनिक सामाजिक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में किसी भी विधि का निर्धारण आदर्श की ओर ध्यान दिये बिना किया जा सकता है अतः विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की वैधानिक आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय को ध्यान दिये बिना आज की जटिल समस्याओं से नहीं निपट सकती है।
प्रश्न 6. (क) विधिशास्त्री के रूप में ऑस्टिन और केल्यान की तुलना कीजिए और अन्तर दर्शाइये।
Compare and contrast Austin and Kelson as jurists.
(ख) “विधि लोगों की आत्मा के अनुरूप होनी चाहिए।” भारत के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।
“Law should be in consonance with the spirit of the people”. Comment with reference to India.
उत्तर (क)- ऑस्टिन और केल्सन के विधि सम्बन्धी विचारों में निकट साम्य है। केल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कान्ट (Kant) के विधि दर्शन पर आधारित किया। किन्तु ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक पद्धति उपयोगितावाद (Utilitarianism) पर आधारित है। निम्नलिखित शीर्षकों में हम ऑस्टिन और केल्सन की तुलना कर सकते हैं-
(1) प्राकृतिक विधि का विरोध – केल्सन और ऑस्टिन दोनों ने ही प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त की कटु आलोचना की है। इसी आधार पर केल्सन और ऑस्टिन को कान्ट और बेंथम से संबंधित किया जा सकता है। केल्सन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया था, क्योंकि ऑस्ट्रियन सिविल कोड जो 1811 ई० से 1911 ई० तक लागू रहा, उस समय बनाया गया था जब प्राकृतिक विधि अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर थी, किन्तु ऑस्टिन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया था, क्योंकि विधि के साथ न्याय को भी संयुक्त कर दिया गया था।
(2) ‘है’ और ‘चाहिए’ में अन्तर- ऑस्टिन एवं केल्सन दोनों ने ही ‘है’ और ‘चाहिए’ में अन्तर स्थापित किया है। ‘है’ का क्षेत्र प्राकृतिक विज्ञान (जैसे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) का क्षेत्र है जबकि ‘चाहिए’ का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान का (जैसे नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, विधिशास्त्र आदि) क्षेत्र है। ऑस्टिन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधिशास्त्र की सीमा से अलग इस कारण बताया क्योंकि उसके नियम राज्य के द्वारा आरोपित नहीं होते। केल्सन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधिशास्त्र से अलग इस कारण रखा क्योंकि वे अस्तित्वमय जगत में कार्य कारण के नियमों पर आधारित हैं अतः दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि विधि वह है जो वास्तव में है। विधि वह नहीं है जो उसे होना ‘चाहिए’ किन्तु साथ ही साथ दोनों ही ने इस बात को स्वीकार किया कि ‘है’ का क्षेत्र केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान के ‘है’ से विधि शास्त्र का अध्ययन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
(3) विधिशास्त्र का क्षेत्र- ऑस्टिन की पद्धति आधुनिक विकसित विधि व्यवस्थाओं का आधार लेकर ही बनायी गयी है। अतः ऑस्टिन ने जिन विचारधाराओं का निरूपण किया है उनमें से अधिकतर इंग्लैण्ड की विधि-व्यवस्था में मान्यता प्राप्त विचारधारायें हैं। अतः ऑस्टिन की पद्धति में सार्वभौमिकता के गुण का अभाव है, किन्तु इसके विपरीत, केल्सन ने जिस पद्धति का विवेचन किया है वह सार्वभौमिक मान्यता के गुण से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त केल्सन की पद्धति शुद्ध (Pure) होने का दावा करती है। शुद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि पद्धति किसी विशिष्ट विधि व्यवस्था के तथ्यों से अप्रभावित रहे। पद्धति को शुद्ध रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह ‘आन्तरिक तथ्यों’ और विशिष्टता पर आधारित हो, और सभी प्रकार के बाहा तथ्यों से पूर्णरूपेण उन्मुक्त हो। किसी विशिष्ट विधि व्यवस्था के संदर्भ में बनायी गयी पद्धति में सार्वभौमिकता का गुण नहीं आ सकता।
(4) आदेश – ऑस्टिन का कथन है कि ‘आदेश’ मानवीय इच्छाओं की मात्र अभिव्यक्ति है। केल्सन महोदय कहते हैं कि हो सकता है कि ‘आदेश’ मानवीय इच्छा की अभिव्यक्ति हो फिर भी वह अभिव्यक्ति ही तो है श्रेष्ठतर (Superior) की इच्छा नहीं। श्रेष्ठतर की ‘इच्छा’ को ही हम महत्व प्रदान कर सकते हैं उसकी अभिव्यक्ति को नहीं। किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति का परिपालन विधिक मनोवैज्ञानिक तत्वों (जैसे जनता द्वारा अनुकरण की स्वाभाविक आदत) से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कोई भी अभिव्यक्ति ‘श्रेष्ठ’ इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती। सामान्य रूप से विधि का कोई भी नियम उस दशा में पारित हुआ समझा जाता है जब उसके पारित होने की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। चाहे उसके पारित करने वाले बहुमत के कुछ या अधिकांश सदस्यों को नियम के आन्तरिक विषयों का बिल्कुल ही ज्ञान न हो अपनी इच्छा को न जानने पर उसकी अभिव्यक्ति’ कोई कैसे कर सकता है। इसके अतिरिक्त विधि के किसी नियम के विपक्ष का अल्पमत, उसके पारित होने में अपनी ‘इच्छा’ की ‘अभिव्यक्ति’ नहीं कर सकता। किन्तु किसी विधेयक के पारित होने में अल्पमत का बड़ा महत्व होता है। उस नियम को विधि का रूप धारण करने के लिए अल्पमत का भी हाथ बंटाना आवश्यक होता है।
(5) ऑस्टिन की ‘स्थिरता’ और केल्सन की ‘क्रियाशीलता‘ – केल्सन महोदय ने स्वयं अपनी ‘शुद्ध’ पद्धति और ऑस्टिन की पद्धति के एक सर्वाधिक ‘विरोध’ की ओर हम लोगों का ध्यान केन्द्रित किया है-
ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणात्मक पद्धति विधि को, नियमों की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में मानती है, जो कि अपने सृजन की प्रक्रियाओं को ध्यान में बिना लाए ही अपने सर्वांगीणरूपेण पूर्ण एवं प्रयुक्त होने के लिए क्षम्य है, किन्तु यह विधि का स्थिर सिद्धान्त है। ज्ञान का ‘शुद्ध’ सिद्धान्त इस बात की आशा करता है कि वह स्थिर होने के साथ-साथ क्रियाशील भी हो, अर्थात् उसके सृजन की प्रक्रियाओं का भी साथ-साथ अध्ययन किया जाय। कारण यह है कि विधि मानकों की किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के विपरीत स्वयं अपने सृजन की प्रक्रियाओं को भी नियन्त्रित करती है।
(6) विधि का स्त्रोत – ऑस्टिन विधि को राज्य अथवा प्रभुसत्ताधारी की देन मानते हैं विधि या प्रभुसत्ताधारी नहीं। किन्तु केल्सन महोदय का कथन है कि राज्य और प्रभुसत्ताधारी किसी विधि व्यवस्था के प्रतीक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रभुसत्ताधारी राज्य और विधि के बीच कोई द्वयभाव (duality) नहीं है। राज्य और कानून में कोई अन्तर नहीं है।
(7) ‘आचार’ की मान्यता- ऑस्टिन आचारों एवं रीतिरिवाजों को कानून समझते ही नहीं, वे व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कानून में स्पष्ट भेद स्थापित करते हैं। किन्तु इसके विपरीत केल्सन अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी लोकप्रिय आचार को भी व्यवस्था के किसी बिन्दु पर ‘मानक’ का रूप प्रदान करके, इस रूप में उसे बंधनकारी स्वभाव प्रदान कर सकता है कि ‘जो कुछ आचार द्वारा प्रतिष्ठापित है। उसका अनुसरण किया जाना चाहिए।’
(8) अनुशास्ति का महत्व – ऑस्टिन के कथनानुसार, कानून की मान्यता या वैधता उसकी ‘अनुशास्ति’ में निहित है, किन्तु केल्सन महोदय अनुशास्ति के स्वरूप को स्वीकार करते हैं।
(9) अन्तर्राष्ट्रीय विधि – ऑस्टिन महोदय अन्तर्राष्ट्रीय विधि को कानून मानते ही नहीं, वह उसे सुस्पष्ट नैतिकता के नाम से पुकारते हैं, किन्तु केल्सन अन्तर्राष्ट्रीय विधि को ‘कानून’ की संज्ञा देने के साथ-साथ उसे प्रादेशिक म्युनिसिपल कानून से उच्चतर रूप प्रदान करते हैं।
(10) ऑस्टिन की पद्धति में विशिष्टता का अभाव- ऑस्टिन महोदय की पद्धति का क्षेत्र विधि के सामान्य नियमों तक ही सीमित है। वह विधि की परिभाषा में उन समस्त नियमों को बहिष्कृत करते हैं जो कि एक ही व्यक्ति या किसी एक ही घटना की ओर लक्षित है। इसके विपरीत केल्सन का मानकों का महत्व कार्यान्वित होने के निम्नतम चरण, विधिक निष्पादन और निर्णय की संतुष्टि तक आकर नीचे उतरते हैं।
उत्तर (ख)- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के सुचारु रूप से चलने और कार्य करने हेतु कतिपय नियमों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों द्वारा उसका पालन आवश्यक होता है। इन नियमों को ही विधि अथवा कानून कहा जाता है। मानव समाज के नियमों को उनकी अनुरूपता में होना चाहिए और दूसरे, समाज का कल्याण इनका ध्येय है अर्थात् विधि लोगों की आत्मा के अनुरूप होनी चाहिए। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों और दशाओं के अनुसार विधि का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानव अधिकार की परिभाषा में कहा गया है- “मानव अधिकार में प्राण स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।” विधि स्वयं में साध्य नहीं होता बल्कि यह एक साधन और उपकरण है, समाज में न्याय प्राप्त करने का उपकरण है। विधि को सामान्य रूप से मान्य सामाजिक सिद्धान्तों एवं स्थापित नैतिक मूल्यों की यथासम्भव अनुरूपता में होना चाहिए। विधि को आवश्यक रूप में निष्पक्ष होना चाहिए। यह किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिये नहीं बनायी गयी होती है। यह सब व्यक्तियों के लिए समान होती है। निष्पक्षता भी विधि का एक लक्ष्य है तथा न्यायालय को भी न्याय, साम्या, युक्तियुक्त और सद्विवेक के नियमों के आधार पर ही इसका निर्वचन करना चाहिए।
प्रश्न 7. (क) प्राकृतिक विधि का क्या अर्थ है? प्राकृतिक विधि के मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय संविधान के निर्माण में प्राकृतिक विधि का क्या योगदान रहा है?
What is meant by Natural Law? Explain the theories of Natural Law. What is contribution of Natural Law in construction of Indian Constitution.
(ख) प्राकृतिक विधि के महत्व को बतलाते हुए सेन्ट थॉमस एक्वीनास के योगदान को भी उल्लिखित कीजिए।
उत्तर (क)- प्राकृतिक विधि का अर्थ (Natural Law-What it means) – प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय प्राचीन यूनान से हुआ। अरस्तू के पश्चात् यूनान में स्टोइक विचारधारा (Stoic Phylosophy) ने जोर पकड़ा। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार विश्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीव और मनुष्य सभी के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। उन्होने इन सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को “प्राकृतिक विधि” की संज्ञा दी। प्राकृतिक विधि के सम्बन्ध में एक विचारधारा यह भी रही है कि जिस प्रकार शासक किसी निश्चित समुदाय पर शासन करता है तथा अपनी व्यावहारिक विवेक बुद्धि के कुछ आदेशों को निर्मित करता है, उसी प्रकार ईश्वर समस्त ब्रह्मण्ड पर शासन करता है तथा ईश्वरीय बुद्धि से उत्पन्न कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। शासक द्वारा निर्मित आदेशों को वास्तविक या सूत्रबद्ध विधि कहां जाता है जबकि ईश्वरीय नियमों को दैवी या प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी गई है। विधिवेत्ताओं ने प्राकृतिक नियमों को विधि के आदर्श मानते हुए यह मत व्यक्त किया कि मानव द्वारा निर्मित ऐसे सभी सूत्रबद्ध कानून (अर्थात् वास्तविक विधि या राजकीय विधि) जो प्राकृतिक विधि के विरुद्ध हैं, अनुचित होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक विधि ही सामान्य विधि (Ordinary Law) को मान्यता या अमान्यता प्रदान करती है।
कालान्तर में प्राकृतिक विधि का क्षेत्र अधिक व्यापक होने लगा। प्राकृतिक विधि- सिद्धान्त सम्बन्धी यह प्राचीन धारणा कि यह सिद्धान्त एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रस्थापना ‘प्रकृति’ (या ईश्वर) से हुई है, समय के साथ धूमिल पड़ने लगी तथा अब इस सिद्धान्त को नैतिकता से सम्बद्ध कर दिया गया है अर्थात् अब प्राकृतिक विधि का सम्बन्ध मनुष्य में पायी जाने वाली मूल प्रवृत्तियों से स्थापित किया गया है।
विधि-विचारकों की दृष्टि में प्राकृतिक विधि के आधार स्रोत भिन्न-भिन्न होने के कारण उन्होंने इसे अनेक नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वर-प्रदत्त मानने वाले विधिशास्त्रियों ने इसे ‘दैव-विधि’ की संज्ञा दी है जबकि इसके सार्वलौकिक स्वरूप के कारण कुछ विद्वानों ने इसे ‘सार्वलौकिक विधि’ भी कहा है। अनेक विधिशास्त्रियों ने इसे नैतिक विधि (Moral Law) तथा अन्य इसे ‘प्राकृतिक विधि’ कहना उचित समझते हैं, क्योंकि यह मानव की नैसर्गिक तर्क शक्ति की उपज है।
प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त
(Theories of Natural Law)
प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त को ऐतिहासिक रूप में मोटे तौर पर चार वर्गों में बाँटा जा सकता है-
(1) प्राचीन सिद्धान्त;
(2) मध्यकालीन सिद्धान्त;
(3) पुनर्जागरण काल के सिद्धान्त; और
(4) आधुनिक सिद्धान्त।
(1) प्राचीन सिद्धान्त
प्राकृतिक विधि-सिद्धान्त का दर्शन सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों की विचारधारा में मिलता है। हेराक्लिटस के विचार में प्रकृति वस्तुओं का विखरा हुआ बेर मात्र नहीं है अपितु प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक सम्बन्ध है। जिस प्रकार प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था है उसी प्रकार मनुष्यों को भी प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव समाज में व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। स्टोइक (Stoic) विचारधारा के अनुगामियों में सुकरात का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने न्याय के दो प्रकार बताये जिन्हें प्राकृतिक न्याय तथा विधिक न्याय की संज्ञा दी गई। प्राकृतिक न्याय सभी स्थानों में एक समान होता है परन्तु विधिक न्याय मूल रूप में हमेशा एक ही प्रकार का होते हुए भी समय और स्थान के साथ-साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है। रोमन-विधिशास्त्रियों ने बाह्य निरीक्षण के आधार पर जिन विधिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया, वे प्राकृतिक विधि के सिद्धान्तों से कुछ मामलों में भिन्न थे। जैसे- दास प्रथा का समर्थन। रोमन विधिशास्त्रियों ने ऐसी विधियों को प्राकृतिक विधि न कहकर सार्वजनिक विधि की संज्ञा दी। ये नियम सार्वभौमिक थे तथा सभी स्थानों या समय में लागू किये जा सकते थे। अन्धयुग (Dark Age) के विचारकों ने प्रकृति के अलावा ‘ईश्वर’ को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना।
(2) मध्यकालीन सिद्धान्त
मध्यकालीन कैथोलिक दार्शनिकों और धर्माचार्यों ने ‘प्राकृतिक विधि’ का एक नवोन सिद्धान्त प्रस्तुत किया। सेंट थॉमस एक्वीनास ने प्राकृतिक विधि को दैवी विधि से पृथक करने का प्रयास किया। उनका विचार था कि यह निर्विवाद है कि ‘दैवी विधि, सर्वश्रेष्ठ है’ परन्तु सम्पूर्ण दैवी विधि का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। मनुष्य दैवी विधि के केवल कुछ भाग को ही जान सकता है जिसे हम प्राकृतिक विधि कह सकते हैं अर्थात् मानव द्वारा निर्मित विधि का ही एक अंश है। इस दृष्टिकोण से एक्वीनास ने विधि के चार प्रकार बताएँ हैं- (1) दैवी विधि; (2) प्राकृतिक विधि; (3) मानवीय विधि; तथा (4) धार्मिक ग्रन्थों में लिखित विधियाँ (Law Divine) तथा सेन्ट थॉमस एक्वीनास ने प्राकृतिक विधि के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए चर्च एवं सम्राट लौकिक एवं पारलौकिक तथा धनवान एवं धनहीन के बीच, जो समन्वय स्थापित किया, वह वास्तव में सराहनीय है।
(3) पुनर्जागरण-काल के सिद्धान्त (Renaissance Theories)
इस काल में अब ईश्वरीय विधि की पारलौकिक शक्ति के स्थान पर मनुष्य की तार्किक बुद्धि को प्राकृतिक विधि का आधार माना गया। प्राकृतिक विधि की इस नवीन व्याख्या का श्रेय प्रसिद्ध डच विधिशास्त्री ह्यूगो ग्रोशियस (Hugo Grotious) को है जिन्हें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रणेता माना जाता है। ग्रोशियस ने सामाजिक संविदा के सिद्धान्त को एक ऐतिहासिक तथ्य मानते हुए इसका निरूपण दो उद्देश्यों से किया। प्रथम यह कि प्रजा प्रत्येक स्थिति में सरकार के आदेशों को माने तथा द्वितीय यह कि राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्बन्ध वैधानिक नियमों पर आधारित हो, परन्तु ग्रोशियस का मत था कि शासक के लिए प्राकृतिक विधि का अनुसरण करना अनिवार्य है। थॉमस हाब्स ने भी सामाजिक संविदा के सिद्धान्त को अपनी राजनीतिक विचारधारा का आधार बनाया। हॉब्स ने आत्म-रक्षा के अधिकार को प्राकृतिक विधि का मूल सिद्धान्त माना है। इन्होंने प्राकृतिक विधि की बजाय नागरिक विधि को ही गुरुतर माना है। मानवीय विधि को राज्य द्वारा निर्मित माना है जिसके पीछे राज्य की शक्ति छिपी रहती है। अतः शासक की सम्प्रभु-शक्ति को स्वीकार करते हुए चर्च को उसके अधीनस्थ माना। जॉन रूसो ने लोकतंत्र का समर्थक होने के कारण व्यक्तिगत निरंकुश शासन का विरोध करने के लिए सामाजिक संविदा के सिद्धान्त का सहारा लिया। उनके विचार में राज्य शक्ति जनता की सामान्य इच्छा (General Will) पर आधारित होनी चाहिए अर्थात् राज्य प्रभुसत्ता सामूहिक रूप से जनता में निहित होती है।
(4) आधुनिक सिद्धान्त
उन्नीसवीं शताब्दी सामान्यतः प्राकृतिक विधि सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी। राष्ट्रवाद तथा विज्ञानवाद के कारण पाश्चात्य जगत में विधि दर्शन की प्रगति में गतिरोध उत्पन्न हो गया। लोगों में भ्रम फैल गया कि विज्ञान की सहायता से आर्थिक प्रगति करने में ही उनका वास्तविक सुख है। विधि के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण औपचारिकताओं से युक्त अनम्य विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का उदय हुआ।
बीसवीं शताब्दी जिसे प्राकृतिक विधि-सिद्धान्तों के पुनरुत्थान (revival) का काल कहा गया है, इस सदी के प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों ने पाश्चात्य देशों की आँखें खोल दी। प्राकृतिक विधि को अब समय और स्थानानुसार परिवर्तित माना जाने लगा तथा वह वाह्य एवं सापेक्ष मानी गयी। प्राकृतिक विधि की इस नई और परिवर्तित संकल्पना को ‘परिवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि’ (Natural Law with variable contents) कहा गया है। डेल वैकिहो के अनुसार प्राकृतिक विधि कानून के विकास से संबंधित एक ऐसा सिद्धान्त है जो मानव जाति को अधिक स्वायत्तता की ओर विकासोन्मुख करता है। स्टेमलर (Stammler) के अनुसार विधि निश्चित रूप से मानव की संकल्प शक्ति है। इस विधि का संबंध बाह्य भौतिक जगत् के क्रिया-कलापों से नहीं है अपितु इसका कार्य साध्य और साधनों को एक-दूसरे से सम्बन्धित करना है।
प्राकृतिक विधि के विषय में विधिवेत्ताओं की धारणाएँ समय के साथ परिवर्तित होती रही हैं। कभी इसका प्रयोग धर्मतन्त्र के समर्थन के लिए किया गया तो कभी-कभी निरंकुश शासन को समर्थन देने के लिए। यूरोप की अनेक राजनीतिक क्रान्तियाँ भी प्राकृतिक विधि के आधार पर हुई। व्यक्तिवाद और प्रत्यक्षवाद की संकल्पनाओं को भी प्राकृतिक विधि के आधार पर ही विकसित किया गया। आज इन सिद्धान्तों की झलक प्रायः सभी न्याय प्रणालियों में देखने को मिलती है।
भारतीय संविधान के निर्माण में प्राकृतिक विधि- भारत में अनेक विधि-सिद्धान्तों और संकल्पनाओं को इंग्लैण्ड से लिया गया है जिनमें से अनेक ‘प्राकृतिक विधि’ पर आधारित हैं, जैसे-संविदा कल्प, अपकृत्य में युक्तियुक्तता, न्याय, साम्या इत्यादि। भारतीय संविधान में प्राकृतिक विधि के अनेक सिद्धान्त समाविष्ट हैं। यह कतिपय बुनियादी स्वतन्त्रताओं अर्थात् मूल अधिकारों की गारण्टी करता है। यह उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को प्रशासनिक और न्यायिक कल्प अधिकरणों पर नियंत्रण रखने को सशक्त करता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 331 में समाविष्ट है जो कहता है कि किसी असैनिक सेवा के सदस्य को तब तब पदच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारें में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही दे खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गाँधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा एम० सी० मेहत्ता वनाम यूनियन आफ इण्डिया, (1999) 6 एस० सी० सी० जैसे वादो के
निर्णयों से प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त क्रमशः न्यायिक कार्यवाहियों का एक मूलभूत अंग बन गया है। आर० एल० शर्मा बनाम मैनेजिंग कमेटी डॉ० हरिराम एच० एस० स्कूल, ए० आई० आर० 1993 एस० सी० में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया- “प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त आधारभूत और मूलभूत संकल्पनाएँ हैं और अब यह विधि निश्चित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के अंग हैं।”
उत्तर (ख) – प्राकृतिक विधि का महत्व – विधि के क्षेत्र में प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त का पर्याप्त महत्व रहा है। रोम की सिविल विधि को व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राकृतिक विधि का ही सहारा लिया गया था। इसी प्रकार मध्य युग में जर्मनी में चर्च और राज्य के बीच आपसी संघर्ष के समय इन दोनों ही पक्षों ने प्राकृतिक विधि का उपयोग एक शास्त्र के रूप में किया तथा स्वयं को दूसरे पक्ष की तुलना में श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वैधता तो प्राकृतिक विधि-सिद्धान्त पर ही आधारित है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के लिए राज्य की असीमित अधिकार शक्ति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विचारकों ने प्राकृतिक विधि को ही अपनी विचारधारा का आधार बनाया। अमेरिका के न्यायाधीशों ने अमेरिकी संविधान के निर्वचन में प्राकृतिक विधि के नियमों का सहारा लेते हुए विधान मण्डल द्वारा मनुष्य की आर्थिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्धों का विरोध किया।
विभिन्न राष्ट्रों के विकास में भी प्राकृतिक विधि-सिद्धान्त का पर्याप्त योगदान रहा है। इस विधि के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विधिवेत्ताओं ने महत्वपूर्ण राजनैतिक, समाजशास्त्रीय तथा वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये जो समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक थे। विधिशास्त्रियों ने प्राकृतिक विधि को अपनी विचारधाराओं के अनुसार अनेक भागों में विभक्त किया है। तद्नुसार प्राकृतिक विधि को प्राधिकारिक तथा व्यक्तिवादी प्रगतिशील तथा रूढ़िवादी धार्मिक तथा विवेकशील निरपेक्ष तथा सापेक्ष आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परन्तु न्यायिक दृष्टि से प्राकृतिक विधि से तात्पर्य ऐसे आदर्श नियमों से है जो राज्य की वास्तविक सूत्रबद्ध विधि की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट और व्यावहारिक हों तथा जिनका वास्तविक विधि द्वारा अनुकरण किया जाना अपेक्षित है।
विचारों का समावेश प्रमुखता से दिखलाई देता है। यह एक ऐसी सर्वव्यापी व्यवस्था है। जो सभी मनुष्यों के प्रति समान रूप से लागू होती है।
सेण्ट थॉमस एक्वीनास का योगदान – प्राकृतिक विधि के सन्दर्भ में सेण्ट थॉमस एक्वीनास का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होनें प्राकृतिक विधि को दैवी विधि से पृथक करने का प्रयास किया। सेण्ट एक्वोनास का विचार था कि समस्त मानव समुदाय दैवी शक्ति द्वारा प्रशासित होता है। यह निर्विवाद है कि दैवी विधि सर्वश्रेष्ठ है परन्तु सम्पूर्ण दैवी विधि का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। मनुष्य दैवी विधि के केवल कुछ भाग को ही जान सकता है जिसे हम प्राकृतिक विधि कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विधि दैवी विधि का ही एक भाग है जिसे मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि द्वारा स्वयं जान सकता है। मानव में बुद्धि या तर्क-शक्ति होने का कारण वह दैवी विधि के इस भाग को अर्थात् प्राकृतिक विधि को, अपने दैनिक जीवन के क्रिया-कलापों में प्रयुक्त कर सकता है और इसके आधार पर उचित-अनुचित का निर्णय ले सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सभी विधिर्या प्राकृतिक नियमों पर ही आधारित हैं। सारांश यह है कि मानव द्वारा निर्मित विधि प्राकृतिक विधि का एक ही अंश है। इस दृष्टिकोण से एक्वीनास ने विधि के निम्नलिखित चार प्रकार बताये हैं-
(1) दैवी विधि (Law of God)
(2) प्राकृतिक विधि (Law of Nature)
(3) मानवीय विधि (Human Laws)
(4) धार्मिक ग्रन्थों से लिखित विधियाँ।
थॉमस एक्वीनास का आग्रह था कि मानव द्वारा बनाये गये कानून प्राकृतिक विधि.तथा दैवी विधि के अनुकूल होने चाहिए। दैवी विधि क्या है, इसका निर्णायक चर्च का पोप था न कि राज्य का शासक। इस प्रकार एक्वीनास ने दोहरी सार्वभौमिक सत्ता का समर्थन किया जो कालान्तर में गम्भीर विवाद का कारण बन गया। सेन्ट थॉमस एक्वीनास के अनुसार मुनष्य द्वारा निर्मित विधि समय और स्थान के अनुसार परिवर्तनशील होती है। यह विधि मूलतः प्रतियोगिता पर आधारित है। केवल वही मानवकृत विधि मान्य हो सकती है, जो प्राकृतिक और धार्मिक विधि की सीमाओं के अन्तर्गत बनाई गई हो। उनका कहना था कि राज्य द्वारा बनाये गये कानून अनुचित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार पारलौकिक क्षेत्र में चर्च की प्रतिष्ठा को प्रधानता देते हुए लौकिक क्षेत्र में उन्हें शासक की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार किया।
थॉमस एक्वीनास ने सम्पत्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए मनुष्य के साम्पत्तिक अधिकारों का समर्थन किया। उनका विचार था कि सम्पत्ति का अर्जन उचित है क्योंकि मनुष्य स्वयं के लिए प्राप्त वस्तुओं के प्रति अधिक जागरूक रहता है जबकि सम्मिलित सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति उतना सजग नहीं रहता। मनुष्यों के बीच सम्पत्ति का विभाजन वस्तुओं की उपादेयता में वृद्धि करता है। सम्पत्ति-प्राप्ति से मनुष्य में संतोष मिलता है जो शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होता है।
सेन्ट एक्वीनास के विचार से मनुष्य में सम्पत्ति के कारण उत्पन्न अमीर-गरीब का भेद- भाव उचित है। किन्तु उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति से पूर्णतः वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। सम्पत्ति का उपयोग केवल प्राप्तकर्त्ता के लिए नहीं, वरन् सभी के हित में किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक विधि के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए मध्य युग के महान दार्शनिक सेन्ट थॉमस एक्वीनास ने चर्च एवं सम्राट, लौकिक एवं पारलौकिक तथा धनवान एवं धनहीन के बीच जो समन्वय स्थापित किया, वह वास्तव में सराहनीय है।
प्रश्न 8. (क) ऐतिहासिक विचारधारा के उद्गम के कारणों की विवेचना कीजिए तथा विधिशास्त्रीय विचार में उसके योगदान का मूल्यांकन करें।
Discuss the causes of origin of Historical School. Evaluate the contribution of this school in Jurisprudential thought.
अथवा (OR)
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के मुख्य लक्षणों (विशेषताओं) की विवेचना कीजिए। विधि के विकास में लोक चेतना (वोकजिस्ट Volkgeist) के महत्व पर प्रकाश डालिए।
Discuss the special characteristics of Historical School of Jurisprudence. Discuss the importance of ‘Volkgeist’ (Peoples. Spirit) in development of law.
(ख) “प्रगतिशील समाज का विकास अब तक प्रास्थिति से संविदा की ओर हुआ है।” सर हेनरी मेन के उपरोक्त विचार का परीक्षण कीजिए। “The movement of progressive societies hitherto has been from status to contract.” Explain the above thought of Sir Henry Main.
(ग) सैविनी और मेन के विचारों की भिन्नता पर प्रकाश डालिए। Elucidate the differences between the thoughts of Savigny and Main.
उत्तर (क)- सैविनी एक जर्मन विधिशास्त्री था। वह उन्नीसवीं शताब्दी का महान विधिशास्त्री था। सैविनी (Savigny) को ऐतिहासिक विचारधारा (Historical School) का संस्थापक माना जाता है। सैविनी ने लोक चेतना (Volkgist) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। Volk (वाक) का अर्थ है लोक या जनता तथा Geist (जिस्ट) का अर्थ है चेतना। सैविनी की विचारधारा को गुस्टाव हागो (Gustav Hugo) द्वारा पूर्व अनुमानित किया गया। सैविनी तथा ट्यूगो का विचार था कि विधि लोकभाषा (Language of people) की भाँति विकसित होती है। लोक भाषा तथा लोक आचार समाज में विकसित होता है। इसका समाज में एकाएक अस्तित्व नहीं होता। यह कालखण्डों में विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत अस्तित्व में आती है। इसी प्रकार विधि सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिरोपित नहीं की जाती। विधि समाज में क्रमिक विकास को प्रक्रिया के अन्तर्गत अस्तित्व में आती है, क्योंकि विधि यदि लोगों द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी तो भारी से भारी शास्ति या दण्ड उसके पालन को सुनिश्चित नहीं करवा सकता। विधि की स्वीकार्यता लोगों द्वारा इसे अपनाने पर निर्भर करती है। समाज में एक आचरण या लोकाचार अस्तित्व में आता है तथा एक क्रमिक विकास (Development) के माध्यम से इसका विकास होता है तथा काफी समय से एक लोकाचार यदि समाज के अस्तित्व में है तो यह प्रथा का रूप ले लेता है तथा प्रथा (Custom) ही विधि का प्रमुख स्रोत है। प्रथा समाज में यदि स्वीकार्य है तो इसी के अनुरूप विधि समाज में अधिक सरलता से स्वीकार्यता प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार भाषा या लोकाचार राजनीतिक अधिकार या अधिनियमन के माध्यम से अस्तित्व में नहीं आते उसी प्रकार विधि भी राजनीतिक अधिरोपण का विषय नहीं है। विधि की समाज में स्वीकार्यता विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत होती है। विधि पायी नहीं जाती विधि विकसित होती है। विधि लोक चेतना का उत्पाद है।
सैविनी के लोकचेतना (Volkgeist) के सिद्धान्त के प्रमुख तत्व (लक्षण) – फ्रेडिक कार्ल वॉन सैविनी (Friedrich Karl Von Savigny (1779-1861) को ऐतिहासिक विचारधारा का डार्विन (Darwin) माना जाता है। (सी० के० एलन की कृत्ति Law in the Making)। डार्विन ने जीव के विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार आधुनिक जगत एक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित हुआ है। आवश्यकता के अन्तर्गत एक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत जीवों का विकास हुआ। उसी प्रकार सैविनी का विचार था कि विधि का अस्तित्व भी एक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत लोकभाषा तथा लोकाचार की भाँति हुआ। सैविनी की अन्तिम कृति डार्विन की सुप्रसिद्ध कृति (Origin of Specie) के छः वर्ष पहले प्रकाशित हुई तब सैविनी जीवित था। सैविनी द्वारा प्रतिपादित लोकचेतना के सिद्धान्त (Principles of Volkgeist) के प्रमुख तत्व निम्न हैं-
(1) सैविनी के अनुसार विधि ऐसी वस्तु नहीं है जिसे विधायक उत्पन्न करते हैं या मनमाने ढंग से इसमें परिवर्तन करते हैं। विधि की विषय-वस्तु का निर्माण वास्तव में जनता (लोगों) के अतीत से होता है। विधि एकाएक निर्मित नहीं होती। यह एक विकास के माध्यम से अस्तित्व में आती है।
(2) किसी राष्ट्र की विधि किसी सम्प्रभु की आज्ञा (समावेश) या आकांक्षा नहीं है। अपितु विधि प्रत्येक जनजाति या समुदाय की आधिकारिक भावना (instinct of race of community) है अर्थात् विधि समाज में चल रहे विचार प्रवाहों का उत्पाद है।
(3) विधि का निर्माण नहीं होता विधि समाज में (प्रथा के रूप में) पाई जाती है। विधि समाज के लोकप्रिय विश्वास (श्रद्धा), सामान्य अवधारणा, प्रथा, स्वभाव के रूप में पाई जाती है जो विधि के नियम के रूप में विकसित होती है।
(4) भाषा, लोकाचार की भाँति किसी देश की विधि का निर्धारण विशिष्ट राष्ट्र लक्षण के रूप में होता है। इसी राष्ट्र लक्षण को लोक चेतना (Spirit of people ‘volkgeist’) कहा जाता है।
(5) विधि सार्वभौमिक या सामान्य चरित्र की नहीं होती। विधि सदैव विशिष्ट होती है जिसका आधार उस विशिष्ट राष्ट्र के लोगों का भी प्रयास होता है। भाषा तथा लोकाचार की भाँति विधि भी विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट होती है। विधि लोगों के विकास के साथ विकसित होती है तथा लोगों की शक्ति से विधि को शक्ति प्राप्त होती है तथा राष्ट्र जैसे ही अपना पृथक् अस्तित्व समाप्त करता है विधि समाप्त हो जाती है।
(6) सैविनी ने विधायन की अपेक्षा प्रथागत विधि को वरीयता प्रदान की। अतः सैविनी विधिशास्त्री को विधायक से अधिक महत्व देता है, क्योंकि विधिशास्त्री लोकचेतना का प्रतिनिधित्व करता है।
(7) सैविनी विधि की अटूट निरन्तरता पर विश्वास करता था। एक राष्ट्र की विधि उसकी भूतकालीन प्रथा से पृथक् नहीं हो सकती। यही भूतकालीन प्रथा भावी विधि का आधार है।
(8) सैविनी के अनुसार विधि समाज का अविभाज्य अंग है। उसने विधि को सामाजिक प्रक्रिया का अंग माना।
सैविनी ने इस सिद्धान्त को खण्डित किया है कि विधि को प्रकृति ने बनाया है। उनके विचार से विधि राष्ट्रीय चेतना या जनता की बुद्धि की उत्पत्ति है।
सैविनी के सिद्धान्त का जन्म जर्मनी में कुछ राजनीतिक कारणों से हुआ। नैपोलियन के युद्ध के पश्चात् जर्मनी के कानून को संहिताबद्ध रूप प्रदान करने का प्रश्न उठा। इस संहिताकरण के प्रबल समर्थक थे प्रोफेसर ट्रीबाट (Tribuout)। प्रो० ट्रीबाट फ्रेन्च सिविल कोड से बहुत प्रभावित हुए। उसने कहा कि जर्मनी के विभिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि इन अगणित कानूनों को एक तार्किक आधार देकर और उनका सामान्यीकरण करके उन्हें संहिताबद्ध कर दिया जाय। देखने में तो इस समस्या का सामाधान बड़ा सरल सा लगता था, किन्तु वास्तव में इस समस्या के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा था। ये स्थानीय कानून स्थानीय जनता के दिल और दिमाग में, रीति-रिवाज में न जाने कितने दिनों, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के एकदम समाहित थे। अतएव इस नवीनीकरण में एक बड़ा संघर्ष छिपा था। वह संघर्ष था-परम्परा का तर्क के विरुद्ध संघर्ष इतिहास का राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध संघर्ष अपने आप बने हुए, अपने आप विकसित, अनादि काल से चले आये कानून का मनुष्य की शक्ति और आत्म-विवेक के अनुसार स्वेच्छानुसार बनाये जाने वाले कानून के विरुद्ध संघर्ष। सैविनी ने जनता के दिलों में परम्परागत विधियों की दुःखभरी आवाजों को सुना, उनको पहचाना और उसको क्षति से बचाने के लिए संहिताकरण का विरोध करने के लिए मैदान में आ डटे।
सैविनी का कथन है कि कानून अपने में पूरी तौर से अमूर्त सिद्धान्तों का संग्रह मात्र नहीं है। वास्तव में यह किसी विशिष्ट मानव समुदाय (या देश) के व्यक्तियों की आन्तरिक आवश्यकता की सामान्य भवना की अभिव्यक्ति है। यह उन व्यक्तियों के आपसी सहयोग से पैदा हुई चेतना की छाया है। मानव सभ्यता की शुरुआत में कानून के विभिन्न समुदायों ने उन देशों की भाषा, स्वभाव और आकृति के समान अपना एक विशिष्ट रूप धारण कर लिया था। वास्तव में भाषा, स्वभाव, कानून और आकृति का पृथक् अस्तित्व नहीं है, वे एक दूसरे से मिलकर एक हो गये हैं। अतः कानून स्वयं विकसित होता है। यदि इस स्वाभाविक विकास में किसी की हेर-फेर हो जाती है तो इससे देश में कलह और अशान्ति ही होगी तथा कोई लाभ नहीं होगा। सैविनी ने ‘सामान्य अन्तर्चेतना’ को ‘Volksgeist’ कहा है, इसलिए उसका सिद्धान्त ‘अन्तर्चेतना का सिद्धान्त’ (Volkgeist theory) कहा जाता है। उसने कहा है कि .”कानून लोगों के विकास के साथ विकसित होता है। लोगों की ताकत के साथ-साथ ताकतवर बनता है। राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो कानून का विनाश हो जाता है।” यहाँ पर राष्ट्र का अर्थ है-व्यक्तियों का वह समुदाय जो सामाजिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कड़ियों द्वारा उन्हें एक सूत्र में बाँध देता है।
अतः सैविनी के अनुसार कानून का गम्भीर स्रोत सामाजिक दृष्टिकोण और जीवन के तरीके में निहित है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं होता कि आम जनता भी देश के समस्त कानूनों से अपने आप परिचित होती है।
यह बात सभ्यता की शुरुआत में सत्य थी, तब भाषा आदि की भाँति कानून के सिद्धान्त बहुत आसान थे और उनका क्षेत्र बहुत सीमित था। किन्तु समाज के विकास के साथ-साथ कानून भी विकसित होकर पेचीदा हो गया। पहले कानून मानव समुदाय की भीतरी चेतना में निहित था, अब वह समुदाय के प्रतिनिधि विधिशास्त्रियों में आ गया। अतः उपर्युक्त मत का प्रतिपादन करते हुए सैविनी ने वर्तमान कानूनों में दो तत्वों की उपस्थिति को देखा-
(1) राजनैतिक तत्व, अर्थात् कानून के तत्व जो समुदाय की अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब है : तथा
(2) तकनीकी तत्व, अर्थात् वह तत्व जो विधिवेत्ताओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। हर एक कानून में इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है।
अतः सैविनी के सिद्धान्त में हम तीन बातें पाते हैं-
(1) कानून का निर्माण नहीं होता, यह मानव समुदाय की भीतरी चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में स्वयं पाया जाता है।
(2) क्वानून प्रारम्भिक सभ्यता के सामान्य नियमों से विकसित होकर धीरे-धीरे पेचीदा हो जाता है। पेचीदगी की हालत में यह समुदाय की भीतरी चेतना को सीधे ढंग से व्यक्त नहीं करता। यह विधिवेत्ताओं द्वारा व्यक्त किया जाने लगता है।
(3) कानूनों में सार्वभौमिकता नहीं होती। एक ही कानून विश्व में सब जगह नहीं लागू किया जा सकता है। जिस प्रकार हर एक देश की अलग-अलग भाषाएँ होती हैं, अलग-अलग स्वभाव हैं, उसी प्रकार हर एक देश का कानून भी अलग-अलग है। समुदायों की अभिव्यक्तियों में अन्तर होता है।
(4) सैविनी के अनुसार, प्राकृतिक विधि के नैतिक आदेश को विधि की अनुशास्ति के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है, विधि के पीछे वास्तविक अनुशास्ति सांमाजिक दबाव ही है।
अन्तर्चेतना सिद्धान्त की आलोचनाही सैविनी के अन्तर्चेतना के सिद्धान्त की विभिन्न विधिशास्त्रियों ने आलोचना की है, जो इस प्रकार है-
(I) सैविनी के इस कथन का खण्डन करते हुए विधि किसी समाज-विशेष यो समुदाय को इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ऐलन ने कहा है कि यदि कोई ऐसा होता है तो रोमन विधि सम्पूर्ण यूरोप में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यह विधि यूरोप की जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थी। विधिशास्त्री ऐलन ने सैविनी के इस मत का भी खण्डन किया है कि विधि के निर्माण में अधिवक्ता वर्ग का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वे जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐलन के मत के अनुसार, “विधियों तथा पूर्व निर्णयों का निर्माण न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।”
(II) सैविनी द्वारा विधि के प्रति अपनायी गई ऐतिहासिक पद्धति विधिशास्त्र की संकल्पनाओं का खण्डन करती है एवं प्राकृतिक विधि के प्रति विरोध प्रकट करती है, परन्तु यथार्थ में सैविनी का अन्तर्चेतना का सिद्धान्त स्वयं ही बाह्य तथ्यों पर आधारित एक आदर्शात्मक कल्पना मात्र है।
(III) यह कहना उचित नहीं है कि विधि सदा ही जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। कभी-कभी विधि के विकास में व्यक्ति विशेष के योगदान का अधिक महत्व रहता है फिर भी, चाहे वह व्यक्ति विदेशी नागरिक ही क्यों न हो।
(IV) अनेक विधियाँ ऐसी हैं जो शासक अपनी सुविधा के लिए बनाता है तथा वे जन- समुदाय की चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होती है।
(V) अनेक विधियों का निर्माण जनचेतना की अदृश्य अभिव्यक्ति पर आधारित न होकर मानव समूह के आपसी संघर्षों के लिए आवश्यक हो जाता है जो सैविनी के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है।
(VI) सैविनी ने एक ओर तो विधि को जन-समुदाय की अन्तर्चेतना की अभिव्यक्ति माना है किन्तु दूसरी तरफ अपने देश के लिए रोमन विधि का समर्थन किया है।
ऐतिहासिक विधिशास्त्र तथा भारतीय स्थिति (Historical School of Jurisprudence and Indian Position) – विधि निर्माण में प्रथा तथा लोक चेतना की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रयास तथा लोक आचार ही विधि की स्वीकार्यता (स्वीकृति) का आधार है। यह कथन भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की विधि व्यवस्था के लिए सत्य है। भारत में भी यदि किसी विधि को लोक स्वीकृति नहीं मिली तो यह केवल विधि पुस्तकों की विषय वस्तु होती है तथा शास्ति के बावजूद ऐसी विधियों का प्रवर्तन नहीं हो पाता। दहेज उन्मूलन इस कथन की औचित्यता का सजीव उदाहरण है। दहेज उन्मूलन के लिए केन्द्रीय विधायन सन् 1961 से अर्थात् करीब 45 वर्षों से है, परन्तु दूसरा प्रवर्तन भारतीय समाज में न के बराबर है, दुर्भाग्य से दहेज के विरुद्ध लोकमत या लोकचेतना का विकास उतना सबल नहीं है जितना हिन्दू समाज के लिए दहेज की एक विवशता बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण दहेज धनपशुओं के लिए या ऐसा कहें कि विधि निर्माताओं के लिए कोई समस्या नहीं है। दहेज यदि समस्या है तो मध्यम वर्ग के लिए है तथा आज हिन्दू समाज का दुर्भाग्य यह है कि दहेज उन्मूलन के पक्ष में प्रबल लोकचेतना का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी प्रकार सती प्रथा की समस्या है। सती प्रथा के विरुद्ध प्रखर शास्ति या दण्ड का प्रावधान होने के बावजूद भारत में कुछ समाज में सती प्रथा यथावत् है इसका कारण उस समाज की सती प्रथा के पक्ष में प्रबल लोकचेतना का अस्तित्व है।
भारत में लोकचेतना का निर्माण संतों तथा समाज-सुधारकों ने किया। विधवा विवाह के पक्ष में लोकचेतना का निर्माण राजाराम मोहन राय के भगीरथ प्रयत्नों के कारण हुआ। इसी के अनुरूप विधायन (शारदा अधिनियम) का निर्माण हुआ तथा आज विधायन विवाह समाज में स्वीकार किया जा रहा है। विधवा विवाह के लिए निर्मित विधि की सफलता तभी है जब इसे समाज स्वीकार करे। समाज में इसके पक्ष में लोकचेतना (Volkgeist) kgeist) है। यदि स्थिति इसके विपरीत रहती तो विधवा विवाह की विधि भी अन्य कतिपय विधियों की भाँति मृत विधि के रूप में विद्यमान रहती है। लोक चेतना का विकास एक कालखण्ड में होता है। इसके लिए एक लम्बी समयावधि तथा दीर्घ सामाजिक स्वीकार्यता की आवश्यकता है। दहेज उन्मूलन के पक्ष में लोक चेतना के विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। यह जब समाज के बहुसंख्यक वर्ग की स्वीकृति प्राप्त कर लेगी, तभी दहेज उन्मूलन अधिनियम अपनी सार्थकता प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार विधि ऊपर से अधिरोपित कर दी जाती है या अधिनियमित कर थोप दी जाती है तो उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होगी, यह आवश्यक नहीं है। यदि विधि प्रथा के रूप में लोक चेतना के माध्यम से पहले विकसित है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। जिस प्रकार प्रथा विशिष्ट स्थान के लिए विशिष्ट होती है उसी प्रकार विशिष्ट राष्ट्र के लिए विशिष्ट होनी चाहिए। दक्षिण भारत में दहेज समस्या नहीं है, जबकि उत्तर भारत में दहेज सामाजिक बुराई है। अतः दहेज उन्मूलन अधिनियम की आवश्यकता जितनी उत्तर भारत में है, उतनी दक्षिण भारत में नहीं है। सैविनी के अनुसार विधि का विकास आवश्यकता के अनुसार नहीं है।
भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध उन्नीसवीं शताब्दी में (जनमत) लोक चेतना के विकास में आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज का योगदान है। इनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोक चेतना (Volkgeist) बनाने में सहायक हुआ।
भारत में अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के उद्देश्य से वोट बैंक के निरर्थक प्रलोभन से वशीभूत होकर सरकार लोक चेतना (Volkgeist) का निरादर कर रही है। मुस्लिम स्त्रियों के भरण-पोषण का प्रश्नं या समान सिविल कोड की माँग की अनदेखी इसका ज्वलंत उदाहरण है। मुस्लिमों को उनके धार्मिक विधि के अन्तर्गत शासित होने की जिद समान सिविल कोड के निर्माण में बाधक है तथा बहुसंख्यक भावनाओं का अनादर है। ऐसा किसी सिद्धान्त के तर्गत नहीं है, परन्तु मुस्लिम मतों (Votes) को अपने पाले में करने की निरर्थक कोशिश है, क्योंकि ऐसा करने से मुस्लिम मतदाता किसी एक दल के पक्ष में एकजुट मतदान करेंगे इसकी कोई सुनिश्चितता (प्रतिभूति) नहीं है। मतदान कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें जाति एक प्रमुख कारक हाल के वर्षों में बना है।
शाह बानो के वाद (1994) में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम स्त्रियों को इद्दत के पश्चात् भी भरण-पोषण का अधिकारी माना, परन्तु मुस्लिम कठमुल्लाओं ने इस निर्णय को कुरान के प्रतिकूल मानते हुए विरोध किया। मुस्लिम नेताओं के इस आन्तरिक विरोध के कारण तथा तुष्टिकरण की नीति के चलते भारत सरकार ने एक विशेष संशोधन पारित कर शाह बानो के बाद में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय निरर्थक कर दिया। समान दीवानी संहिता आज भी भारत को बहुसंख्यक लोक चेतना है, परन्तु अल्पसंख्यक तुष्टिकरण तथा वोट बैंक की निरर्थक आशा इस लोक चेतना का निरादर कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि अल्पसंख्यक वर्ग को लोक चेतना के माध्यम से समान दीवानी संहिता (Common Civil Code) की आवश्यकता से अवगत करा कर उसके पक्ष में अल्पसंख्यकों की मानसिकता का विकास करना। विश्व के सभी राष्ट्रों में समान विधि सभी नागरिकों पर लागू होती है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यह विडम्बना है।
सर हेनरी मेन तथा ऐतिहासिक विचारधारा (Sir Henry Maine and Historical School)- सन हेनरी मेन (1822-1888) इंग्लैण्ड में ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवक्ता माने जाते हैं। मेन की प्रमुख कृतियाँ हैं- प्राचीन विधियाँ (Ancient Law (1861), निकायों के प्राथमिक इतिहास प्रवचन Lecourt on Early History of Institution (1874) प्राथमिक विधि तथा प्रथाओं पर शोध पत्र Dissertation on Early Law and system (1883)। हेनरी मेन 25 वर्ष की आयु में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में सिविल लॉ का रेगियस प्रोफेसर नियुक्त हुआ। 1861 से 1869 तक भारत में गवर्नर की परिषद में विधि सदस्य था इससे उसे भारतीय स्थितियों का निकट से पूर्ण अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तुलनात्मक विधिशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में भारतीय विधिक संस्थाओं का ज्ञान उसकी महान उपलब्धि थी।
हेनरी मेन ने यह प्रदर्शित कर महान् योगदान किया कि कुछ समय तक पूर्व तथा पश्चिम में विधि तथा विधिक निकायों का विकास एक समान तथा समानान्तर हुआ। भारत में हिन्दू विधि विकसित हो रही थी तो उसी प्रकार की विधि का विकास इंग्लैण्ड तथा अन्य पश्चिम समाज में हो रहा था।
हेनरी मेन के अनुसार भारत तथा यूरोप में रोमनों तथा हिन्दुओं के इतिहास के प्राथमिक चरणों में पितृ प्रधान समाज का अस्तित्व था। परिवार में पुरुष ही सर्वोच्च होता था तथा परिवार की बागडोर उसी के हाथ में होती थी। परिवार के बच्चों, स्त्रियों तथा अन्य छोटे सदस्यों के लिए परिवार के बड़े पुरुष व्यक्ति के शब्द ही, आदेश ही विधि थी। इसके पश्चात् पारिवारिक समूह का विकास हुआ तथा परिवार समूह समाज में प्रमुखता प्राप्त था। रोमन तथा हिन्दू समाज में स्त्रियों को कोई व्यक्तिगत हैसियत प्राप्त नहीं थी।
उत्तर (ख) – विकास के सिलसिले में सर हेनरी मेन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि “प्रगतिशील समाज का विकास अब तक प्रास्थिति से संविदा की ओर हुआ है।” जो समाज अपनी विधि का नवीन रीतियों से विकास करते हैं, वे प्रगतिशील (progressive) कहलाते हैं। प्रगतिशील समाज तीन रीतियों से अपनी विधियों को विकसित करते हैं-
विधिक कल्पितार्थ, साम्या और विधायन द्वारा आगे विकास- विधिक कल्पितार्थ, साम्या और विधायन विधि के शब्दों में कोई परिवर्तन किये बिना, विधि को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। आंग्ल और रोमन विधि में इसके अनेक उदाहरण हैं। साम्या में वे सिद्धान्त होते हैं जो विध्यात्मक (positive) विधि की अपेक्षा अधिक आदर योग्य माने जाते हैं। इसका उपयोग विधि की कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। विधायन सबसे अन्त में आता है जो कि विधि-निर्माण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष और प्रणालीबद्ध रीति होती है।
हैसियत (status) की समाप्ति – विधि के विकास के सामान्य सिलसिले के (स्थिर समुदायों के) अन्त में जो विधिक दशाएँ विद्यमान रहती हैं, मेन उन्हें हैसियत (status) कहता है। समाज के किसी सदस्य के अधिकार और दायित्व, उसके समाज में किसी वर्ग- विशेष के होने पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के लिये कुटुम्ब में किसी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य उसके कुटुम्ब-पिता अथवा आश्रित होने पर निर्भर करते हैं, आदि। प्रगतिशील समाजों में हसियत की कल्पना समाप्त हो जाती है। “कुटुम्ब पर आश्रितता क्रमशः समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर वैयक्तिक बाध्यता (personal obligations) आ जाती है। सिविल विधियों द्वारा विचार में ली जाने वाली इकाई के रूप में कुटुम्ब के स्थान पर व्यक्ति आ जाता है।”
संविदा की कल्पना का जन्म – क्रमशः कुटुम्ब पिता (पेटर फेमिलियास) संस्था समाप्त होती है। दास अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करते हैं, और अब अधिकार और बाध्यतायें संविदा या व्यक्तियों की स्वतन्त्र सौदेबाजी पर निर्भर करती है। विकास के सिलसिले का इस प्रकार विवेचन करने के पश्चात् मेन अपने महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। “प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा पर गए हैं” (The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract).
मेन का सिद्धान्त अपने समय में ठीक था- वस्तुतः अपने सिद्धान्त को बनाते समय मेन की बात बिल्कुल ठीक थी। प्राचीन रोमन विधि के उदाहरणों के अतिरिक्त, अपने काल में इंग्लैण्ड और यूरोपीय महाद्वीप में उसने व्यक्ति की हैसियत से मुक्ति को देखा। इंग्लैण्ड में विवाहित स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। धर्म के आधार पर अनेक नागरिक निर्योग्यताएँ अधिनियमों द्वारा समाप्त कर दी गयीं। संविदा करने के लिए सेवकों को अधिक स्वतन्त्रता दी गयी। औद्योगिक क्रांति ने अनेक कृषक समुदायों को औद्योगिक प्रोलेटेरियट में बदल दिया जिन्हें नियोजक से संविदा करने की स्वतन्त्रता थी। अमेरिकन गृह-युद्ध में मेन ने औद्योगिक उत्तर अमेरिका की, जो अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र संविदा पर आधारित समुदाय था, कृषक और सामंती दक्षिण (अमेरिका) पर, जो अपेक्षाकृत अधिक हैसियत के पक्ष में था और दासता की संस्था को बनाये रखना चाहता था, विजय को देखा। इन सबसे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा की ओर जाता है।
यह सिद्धान्त अब सही नहीं रहा – तत्पश्चात् विपरीत दिशा में गमन (counter- move) प्रारम्भ हुआ जिसके चिह्न स्वयं मेन के समय में प्रकट हो गये थे। यह अनुभव किया गया कि एक शक्तिशाली पूँजीपति और एक भूखे कर्मकार (workman) के बीच संविदा की स्वतन्त्रता हंसी के योग्य और खोखली बात थी। कर्मकारों की संरक्षा करने के लिए संगठन अस्तित्व में आये। नियोजकों ने भी अपने संघ (संगम) बनाये। अब संविदा करने की व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर वर्गगत सौदेबाजी प्रारम्भ हुई।
संविदा करने की व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कमी- इसके अतिरिक्त, बहुत-सा सामाजिक विधान (social legislation) पारित किया गया है जिसमें मजदूरों के काम के अधिकतम घण्टे और न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी गयी है और प्रतिकर (compensation) सम्बन्धी नियम और सेवा की अन्य शर्तें अधिकथित की गयी हैं और व्यक्ति उनसे आबद्ध (bound) है।
राज्य की संकल्पना और कृत्य में परिवर्तन- अब राज्य की संकल्पना और कृत्यों में भारी परिवर्तन हो गये हैं जिससे राज्य द्वारा व्यक्ति के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर हस्तक्षेप बढ़ा है। यहाँ तक कि उन संविदाओं का जिन्हें कोई व्यक्ति अपने प्रतिदिन के जीवन में करता है, मानकीकरण हो गया है, जैसे पानी या विद्युत-प्रदाय के लिये संविदा या किसी रेलवे कम्पनी के साथ गाड़ी की संविदा। व्यक्ति इन संविदाओं की किन्हीं शर्तों को बदल नहीं सकते।
मानव विज्ञान (एन्थ्रोपोलोजी) में आधुनिक शोधों से नये तथ्य प्रकाश में आये हैं जिससे आदिम समाजों और प्राचीन विधि के विकास क्रम के बारे में मेन के बहुत सारे कथन गलत निकले हैं, तथापि आधुनिक मानव विज्ञानियों को मेन और उसके बाद के अन्य विधिशास्त्रियों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने तथा अपने सहकर्मियों द्वारा अनेक दिशाओं में की गई शोधों का लाभ मिला है।
मेन का सिद्धान्त प्रगति में विश्वास की बात कहता है और उसमें सामाजिक चिन्तन के बीज विद्यमान थे। मेटलैण्ड, विनोग्रेडौफ और ब्राईस जैसे विधिशास्त्रियों को मेन से प्रेरणा मिली और उन्होंने विधि के अध्ययन पर उसकी ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति को लागू किया।
उत्तर (ग)- सेविग्नी और मेन के विचारों में भिन्नता – विधि के क्षेत्र में सैविग्नी और ऑस्टिन दोनों का ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। सैविग्नी विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक थे जब कि ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के समर्थक थे। सैविग्नी ने विधि को लोक-चेतना का परिणाम माना है जबकि आस्टिन विधि को सम्प्रभु का समादेश मानते हैं। सैविग्नी और ऑस्टिन के विधि सम्बन्धी विचारों में अन्तर होते हुए भी दोनों प्राकृतिक विधि की श्रेष्ठता के विरोधी थे तथा दोनों ने विधि के प्रति तुलनात्मक पद्धति अपनाते हुए विधि की वास्तविकता को अधिक महत्व दिया, तथापि दोनों में निम्नलिखित असमानताएँ थीं-
(1) सैविग्नी ने रोनन तथा जर्मन विधि को अपनी लोक चेतना का आधार बनाया जबकि ऑस्टिन का आज्ञात्मक सिद्धान्त इंग्लिश विधि पर आधारित है।
(2) सैविग्नी का सिद्धान्त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है जबकि ऑस्टिन ने अपने सिद्धान्त में तर्क को विशेष महत्व दिया।
(3) ऑस्टिन विधि को राज्य की उपज मानते हैं, परन्तु सैविग्नी विधि को राज्य का पूर्ववर्ती मानते हैं।
(4) ऑस्टिन ने ‘शक्ति’ को विधि का आधार बिन्दु माना परन्तु सैविग्नी उसे स्वीकार नहीं करते हैं।
यद्यपि रीविग्नी तथा सर हेनरी मेन दोनों ही विधिशास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक थे परन्तु अनेक बातों में उनके विचार एक-दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ एक ओर सैविग्नी ने प्रथाओं को महत्व दिया वहीं दूसरी ओर हेनरी मेन ने सभ्यता के विकास के साथ विधायन द्वारा निर्मित संहिताबद्ध विधि की आवश्यकता पर बल दिया। अपने तर्क की पुष्टि में हेनरी मेर्ने ने इंग्लैण्ड की तत्कालीन विधि की अस्पष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसका मूल कारण यह था कि यह विधि प्रधान रूप से न्यायाधीशों द्वारा निर्मित की गई थी न कि विधान-मण्डल द्वारा। हेनरी मेन ने सैविग्नी के ‘लोक चेतना के सिद्धान्त’ को मान्य नहीं किया। उन्होंने विधान-मण्डल की सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार किया जिसे सैविग्नी ने भानने से इन्कार कर दिया था। वस्तुततः हेनरी मेन ने प्रगतिशील समाज के लिए विधान को विधि के निर्माण का एक अनिवार्य साधन माना है। उनका “प्रास्थिति से संविदा की ओर का सिद्धान्त व्यावहारिक होने के साथ-साथ तत्कालीन पूँजीवादी और औद्योगिक समाज की परिस्थितियों के लिए उसी प्रकार अनुकूल था जिस प्रकार से सैविग्नी का लोक चेतना का सिद्धान्त तत्कालीन जर्मन समाज की आन्तरिक भावनाओं के अनुकूल था। गद्यपि इन दोनों विधाशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता है फिर भी दोनों को उन मानवीय संस्थाओं की मौलिक दृढ़ता के प्रति विश्वास था जिन पर अधिकांश विधिक इतिहासकार विश्वास करते हैं।”
प्रश्न 9. (क) विधि का कार्य सामाजिक इन्जीनियरिंग है। इस कथन के आलोक में रास्को पाउण्ड के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। The function of law is social engineering. Discuss the theory of Rascoe Pound in the light of this statement.
अथवा (OR)
रास्को पाउण्ड के सामाजिक अभियन्त्रण के सिद्धान्त की व्याख्या करें। Discuss the Social Engineering Theory of Roscoe Pound.
(ख) रास्को पाउण्ड के सामाजिक अभियन्त्रण के सिद्धान्त की सुसंगतता की व्याख्या भारतीय समाज के सन्दर्भ में करें। Discuss the relevancy of Pound’s theory of Social Engineering in the context of Indian Society.
(ग) “उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि विधि एक सामाजिक प्रयोजन और अभियांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको समझे बिना विधि के प्रति न्याय नहीं हो सकता है। विधि जीवित की सेवा के लिए है। यह अपने पंख न्यायिक शून्यता में नहीं फड़फड़ाती है।” टिप्पणी कीजिए। “Judges of the Supreme Court must not forget that law has a social purpose and an engineering process without appreciating which Justice of law cannot be seen, Law is meant to serve the living and does not beat its wings in the Jural void.” Comment.
उत्तर (क)- रास्को पाउण्ड का सामाजिक अभियन्त्रण का सिद्धान्त (Doctrine of Social Engineering of Roscoe Pounds)- रास्को पाउण्ड एक अमेरिकन विधिशास्त्री था। उसका जन्म लिकन नेब्रास्का में हुआ था। 1901 में वह नेब्रास्का में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ। 1903 में वह नेब्रास्का (Nebraska) विश्वविद्यालय के विधि विद्यालय का डीन अधिष्ठाता नियुक्त हुआ। इसीलिए उसे डीन (Dean) रास्को पाउण्ड भी कहा जाता है। 1916 से 1936 तक वह हारवर्ड विश्वविद्यालय में विधिशास्त्र का प्रोफेसर रहा। हारवर्ड से ही उसने सामाजिक विधिशास्त्र पर अपने कई लेख प्रकाशित करवाए। समाजशास्त्रीय विधि के प्रवक्ताओं में डीन रास्को पाउण्ड अग्रणी तथा प्रमुख विधिशास्त्री है। हाल के वर्षों में विधिक विज्ञान के क्रियाशील दृष्टिकोण के विकास के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जा सकता है। उनका मानना है कि विधि क्रियाशील होनी चाहिए न कि आदर्श या अमूर्त या पुस्तकों में लिखो विषय-वस्तु। विधि अपना उद्देश्य प्राप्त करे इसके लिए विधिशास्त्रियों द्वारा संज्ञान, प्रभावशाली एवं कौशलपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। विधिक इतिहास की व्याख्या (Interpretation of Legal History) में पाउण्ड ने कहा विधि, ज्ञान तथा अनुभव का निकाय है जिसकी सहायता से सामाजिक अभियन्त्रण का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। (Law is the body of knowledge and experience with the aid of which large part of social engineering is carried on) विधि नियमों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। विधि के अन्तर्गत निर्णय तथा आचरण के लिए मानक तथा परिकल्पनाएँ हैं। जिस प्रकार एक इंजीनियर के पास कुछ सूत्र होते हैं, विधि के निर्णय तथा आचरण के लिए मानक तथा परिकल्पनाओं में कुछ सिद्धान्त वृत्तिक विचार होते हैं। यह अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रास्को पाउण्ड के विचार में विधिशास्त्र सामाजिक अभियन्त्रण (Social Engineering) का एक विज्ञान (विशेष ज्ञान) हो जाता है जिसका सन्दर्भ सामाजिक सम्बन्धों के क्षेत्र में उस अंश या अंग से है, जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज के कार्यों को नियन्त्रित करने के लिए सक्षम है। सामाजिक अभियन्त्रण के कार्य को सुगम या सरल बनाने के लिए पाउण्ड ने उन हितों का वर्गीकरण किया है जिन्हें राज्य द्वारा संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। राज्य द्वारा जिन हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए उन हितों को पाउण्ड ने तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है-
(1) निजी हित (Individual Interest) – विधि द्वारा संरक्षण के योग्य निजी हित (Private Interest) निम्न प्रकार का है-
(i) व्यक्तित्व से सम्बन्धित व्यक्तिगत हित (Individual Interest of personality)- इसमें व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, इच्छा की स्वतन्त्रता, आत्मा की स्वतन्त्रता सम्मिलित है। इन हितों की सुरक्षा अपकृत्य विधि, आपराधिक विधि, संविदा विधि करती है। इन हितों की सुरक्षा विश्वास तथा यह विचार की विषय-वस्तु में हस्तक्षेप पर, सरकार की शक्तियों पर अधिरोपित सीमाओं द्वारा की जाती है।
(ii) घरेलू सम्बन्धों में व्यक्तिगत हित (Individual Interest in domestic elations)- इसमें पति-पत्नी के, माता-पिता के तथा बच्चों के मध्य सम्बन तथा विवाह को सम्मिलित किया जाता है। इसमें भरण-पोषण प्राप्त करने का हित भी सम्मिलित है।
(iii) वस्तु या सामान का हित (Interest of Substance)- इसमें साम्पत्तिक अधिकार, उत्तराधिकार, वसीयती उत्तराधिकार तथा वृत्तीय स्वतन्त्रता सम्मिलित है।
(2) लोकहित (Public Interest)- लोकहित में (1) हित सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य संरक्षित करता है; तथा (ii) राज्य के हित जिन्हें सामाजिक हित के रूप में राज्य अभिभावक के रूप में संरक्षित करता है।
ऐसे सामाजिक हित जिन्हें विधि संरक्षण की पाउण्ड आवश्यकता समझता है निम्न हैं-
(1) शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा सामान्य सुरक्षा बनाये रखने के प्रयोजन से जो हित राज्य के संरक्षण में हैं।
(2) विवाह तथा धार्मिक संस्थानों जैसी सामाजिक निकायों के लिए संरक्षित हित।
(3) भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करने वाले, जुए को हतोत्साहित करने वाले तथा वर्तमान नैतिकता के विरुद्ध संव्यवहार को अवैध बनाने वाले हित।
(4) शिक्षा की स्वतन्त्रता, वाक् तथा अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता, सम्पत्ति को स्वतन्त्रता, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता की प्रगति तथा प्राप्ति के लिए आवश्यक सामान्य हित।
(5) सामाजिक स्रोतों का संरक्षण करने वाले हित।
(6) मानवीय व्यक्तित्व की प्रगति के लिए आवश्यक हित।
उपरोक्त हितों के सन्तुलन तथा मूल्यांकन के लिए विधिक विज्ञान के समक्ष जो समस्या है, उस समस्या को सुगम बनाने के लिए सभ्य समाज के लिए पाउण्ड ने कुछ विधिक उपधारणा (Postulates) बताये हैं। 1919 में पाउण्ड ने इस उपधारणा को निम्न रूपों से उल्लिखित किया है। सभ्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन उपधारणाओं (Postulates) को उपस्थिति को स्वीकारना होगा।
(1) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जो कुछ भी उसने अपने श्रम से सृजित किया है उसका वह अपने उपयोग के लिए प्रयोग कर सकता है।
(2) दूसरे व्यक्ति उन उपधाराओं पर आशयपूर्ण ढंग से आक्रमण नहीं करेगा।
(3) यह कि दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्तियों के साथ जो, विधिक उपधारणाओं पर कार्य कर रहा है, समुचित सावधानी के साथ कार्य करेगा तथा उसे अनुचित क्षति पहुँचाने का जोखिम नहीं उठायेगा।
(4) जिन लोगों के साथ व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उन्हें भी सद्भावपूर्वक कार्य करना चाहिए।
(5) यह कि ऐसे व्यक्ति को नौकरीशुदा व्यक्ति को भाँति सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए।
(6) यह कि जब विधिक उपधारणा धारण करने वाला व्यक्ति बूढ़ा होगा तो समान को उसकी सुरक्षा का भार वहन करना होगा।
(7) याह कि पूरे समाज को दुर्भाग्य तथा अक्षमता के अदृश्य जोखिम को वहन करना होगा।
विभिन्न हितों का सन्तुलन बनाये रखने के लिए तथा मूल्यांकन करने के लिए विधायकों तथा न्यायाधीशों को उपरोक्त उपधाराओं, नियमों (Postulates) को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायमूर्ति कारडोजो (Cardozo) ने कहा-यदि आप यह जानना चाहते हैं कि एक उपधारणा (Postulates) या नियम दूसरे पर कब भारी पड़ रहा है तो उसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि उसे अपना ज्ञान एवं अनुभव जीवन के अध्ययन का उपयोग करना होगा।
क्रियाशील विचारधारा (Functional School)- समाजशास्त्रीय विचारधारा का आधारभूत तत्व यह है कि हम कोई चीज क्या है इसे तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करते कि वह वस्तु क्या कर रही है। क्रियाशील विधि, पुस्तकीय विधि से पृथक् है। विधिशास्त्रियों से यह आशा की जाती है कि वे विधिक निकायों की वास्तविक कार्य विधि का परीक्षण करें तथा यह देखें कि विधि का उद्देश्य क्या है? विधि क्यों बनी है? इसीलिए पैटन ने समाजशास्त्रीय विचारधारा को क्रियाशील विचारधारा बताया है।
उत्तर (ख)- समाजशास्त्रीय विचारधारा तथा भारतीय परिदृश्य – स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय विधायकों, भारतीय न्यायाधीशों तथा भारतीय विधिशास्त्रियों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ा है। समाज के लिए सामाजिक तथा आर्थिक ध्येय प्राप्त करने के सन्दर्भ में विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा का महत्व काफी बढ़ा है। व्यक्तिगत हितों का सामाजिक हितों के साथ समन्वय बनाये रखने की आवश्यकता में वृद्धि हुई जिससे स्वतन्त्र भारत में सामाजिक हितों, सामाजिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना सम्भव हो सके। 1947 के पूर्व नवीन विधि के निर्माण के समय विधायक, न्यायाधीश तथा विधि प्रशासक समाज में व्याप्त समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे। विधि के प्रति सन् 1947 के पूर्व आज्ञापक (Imperative) विचार की प्रमुखता थी। विधि स्वतन्त्रता के पूर्व ऊपर से अधिरोपित की जाती थी। ऐसी विधियों में भारत भूमि की महक नहीं होती थी तथा इसकी भाषा भी विदेशी होती थी।
सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विधिक प्रतिनिधियों में परिवर्तन आया। स्वतन्त्र भारत में एक ऐसा संविधान स्वीकार किया गया, लागू किया गया जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त करना था। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए नवीन सामाजिक तथा आर्थिक नीतियाँ बनीं। ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक या आज्ञापक या अधिरचित (विधि जैसो है) के दृष्टिकोण को त्याग दिया गया। अब विधि का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति बना क्योंकि नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था। विधि के माध्यम से संघर्षरत सामाजिक हितों के मध्य समन्वय बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। विधि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए विधि सामाजिक विचारधारा के अनुकूल बनी।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय विधिशास्त्र में निम्न परिदृश्य का उदय हुआ-
(1) आधुनिक स्वतन्त्र भारत में न्यायाधीशों, विधायकों तथा वकीलों के लिए आवश्यक हुआ कि वे आज्ञापक सिद्धान्त का पूर्णतः त्याग कर सामाजिक तथा आर्थिक हितों के लिए विधि कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाये।
(2) समाज में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के ध्येयों को प्राप्ति के लिए विधायक को एकमात्र माध्यम माना गया।
(3) भारतीय विधियाँ पश्चिमी विधिक विचारधारा की नकल नहीं होनी चाहिए, न ही यह रूस की हू-ब-हू नकल होनी चाहिए। यह हमारे अपने लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए।
(4) भारतीय संविधान मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त को शामिल सामाजिक परिवर्तन के ध्येय को प्रकट करता है।
(5) विधायकों, सामाजिक नेताओं को योजनाकारों के तथा विधि प्रशासकों के लिए वह आवश्यक है कि वे सामाजिक आवश्यकताओं को खोजें तथा सामाजिक अनियन्त्रण के सिद्धान्त को भारत में लागू करें।
भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सामाजिक ध्येयों को प्राप्त करने के लिए कई विधायन पारित किये गये। कृषि तथा भूमि सुधार, श्रम सुधार, भ्रष्टाचार निरोधक तथा अछूत निवारण विधि, हिन्दू विधि का संहिताकरण जिसके द्वारा महिलाओं को अधिकार दिया जाना, दहेज उन्मूलन अधिनियम, 1961, बोनस भुगतान अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, 1970, अनैतिक व्यापार प्रतिबन्ध अधिनियम, 1986, उपभोक्ता अधिनियम। उपरोक्त समाजशास्त्रीय अधिनियमों के रूप में उल्लिखित किये जा सकते हैं।
सामाजिक अभियन्त्रण तथा भारतीय न्यायालय (Social Engineering and Indian Courts)- भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिलक्षित हुआ है। न्यायालयों ने विधिक अधिनियमों की व्याख्या करते समय ऑस्टिन के विधि जैसी है (Law as it is) के अधिरचनावादी आज्ञापक (Imperative and Enacted Law) के सिद्धान्तों का परित्याग का विधि को सामाजिक सुधार के साधन के रूप में सवीकार किया है। अपने विधिक प्रावधानों की व्याख्या की प्रक्रिया में न्यायाधीशों ने उत्प्रेरक तथा सामाजिक सुधार की भूमिका निभाने में संकोच नहीं किया है। हाल के वर्षों में उच्चतम न्यायालय निर्णय देकर चुप नहीं बैठा है, उसने यह देखने का प्रयत्न क्या है कि उसके द्वारा दिये गये निर्णय लागू हों। चुनाव सुधारों के निमित्त दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है। चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार चुनाव आवेदन पत्र दाखिल करने के कुछ नियम बनाये हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव आवेदन दाखिल करने के समय शपथपत्र द्वारा अपने विरुद्ध लाये गये वादों या कार्यवाही तथा उस साम्पत्तिक ब्यौरे को प्रकट करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है परन्तु दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को तथा चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता को निष्प्रभावी कराने की कवायत प्रारम्भ कर दी है। भारतीय न्यायालयों ने भ्रष्ट राजनेताओं को सजा देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री जयललिता तथा हिमाचल विकास दल के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व संचार मन्त्रों सुखराम का नाम उल्लेखनीय है, परन्तु यह विडम्बना है कि उन लोगों को उच्च न्यायालय द्वारा दौषमुक्त करार दे दिया जा रहा है।
आज भारत गरीबी विरोधी तथा समता मूलक समाज की ओर बढ़ रहा है। भारतीय संविधान में जहाँ कतिपय मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वहीं न्यायालयों द्वारा इन अधिकारों के मनमाने प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है। ऐसा परस्पर विरोधी हितों पर तालमेल स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य नामक बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा कि विचारशील प्राणी होने के कारण मनुष्य बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है परन्तु सामाजिक हितों के साक्षण के पक्ष में उसे अपनी इन इच्छाओं को नियन्त्रित करना होगा।
सामाजिक न्याय के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसे न्यायालयों ने सख्ती से लागू किया है परन्तु अन्य वर्गों का ख्याल रखते हुए यह अभिघटित किया कि आरक्षण पदों की कुल संख्या के 50% से अधिक नहीं हो सकता। बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ए० आई०. आर० 1963 एस० सी० 649)।
रूरल लिटिगेशन एण्ड डेवेलपमेण्ट सेन्टर देहरादून बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए० आई० आर० 1985 एस० सी० 652 नामक बाद में उपजीविका, व्यवहार तथा उद्योग स्थापित करने के अधिकार तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच हितों के परस्पर संघर्ष की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने दोनों हितों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के अधिकार को मान्यता देते हुए उद्योग स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण के उपायों को किया जाना आवश्यक किया। इसके अभाव में उद्योग लगाने के अधिकार को सीमित किया।
इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायालयों का दृष्टिकोण सामाजिक विचारधारा की ओर उन्मुख हुआ।
उत्तर (ग)- उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ का सर्वोच्च न्यायिक अधिकरण है। इसके पास बहुत विस्तृत अपील, रिट, पुनरीक्षणीय और कुछ मामलों में आरम्भिक अधिकारिता भी है। इसके द्वारा घोषित विधि देश के समस्त न्यायालयों पर आबद्धकर है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों को यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि विधि एक सामाजिक प्रयोजन और अभियांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको समझे बिना विधि के प्रति न्याय नहीं हो सकता है। भारत में एक लिखित संविधान है। प्रत्येक कानून को संविधान की समरूपता में होना चाहिए। भारत में अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कानून के निर्वचन में बाहरी सामग्री को भी विचार में लिया है परन्तु उसे ऐसे निर्वचन में विधि के सामाजिक प्रयोजन एवं अभियांत्रिकी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे आधुनिक काल में, यह न्याय तन्त्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसको न्यायपालिका कहा जाता है।
सामाजिक न्याय भारत की विधि प्रणाली की आधारशिला है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सामाजिक न्याय के महत्व को दर्शित किया है और उसकी व्याख्या की है। एयर इण्डिया स्टेट्यूटरी कारपोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन, (1997) 9 एस० सी० सी० 377 के वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना में जो भारत के संविधान में सन्निविष्ट हैं, नाना प्रकार के सिद्धान्त हैं जो प्रत्येक नागरिक के व्यवस्थापूर्ण उन्नयन और विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह सामाजिक न्याय सामान्य अर्थ में न्याय का एक अभिन्न अंग है। न्याय एक सामान्य वर्ग है सामाजिक न्याय जिसका एक प्रकार है। सामाजिक न्याय निर्धनों, दुर्बलों, दलितों, आदिवासियों और समाज के साधनहीन वर्गों के कष्टों का निवारण करने के लिए और उन्हें समता के स्तर पर उठाने के लिए है जिससे वे गरिमापूर्ण रूप से जी सकें। अतः सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता और सुरक्षा विधि का एक मुख्य ध्येय होता है। इसको ध्यान में रखकर ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों को भी अपने पंख न्यायिक शून्यता में न फड़फड़ाकर उन्हें व्यक्तियों की सेवा के लिए अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
प्रश्न 10. समाजशास्त्रीय विचारधारा के उद्गम के कारणों की विवेचना करें। विधिशास्त्र के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय विचारधारा के योगदान का मूल्यांकन करें।
Discuss the causes of origin of Sociological School of Jurisprudence. Evaluate the contribution of Social School of Jurisprudence in the field of Jurisprudence.
उत्तर- समाजशास्त्रीय विचारधारा का उद्भव ऑस्टिन की अधिरचना या आज्ञापक विधिशास्त्र तथा फ्रेड्रिक वॉन कार्ल सैविनी के उदासीन ऐतिहासिक विचारधारा की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। विधि की समाजशास्त्रीय विचारधारा आधुनिकतम विचारधारा है। इसका उद्भव बीसवीं शताब्दी की प्रमुख उपलब्धि रही है। बीसवीं शताब्दी के विधिशास्त्रियों के चिन्तन का मुख्य केन्द्र व्यक्तिगत अधिकार की अपेक्षा सामाजिक दायित्व बना। बीसवीं शताब्दी में विधि की क्रियाशीलता पर अधिक बल दिया जाने लगा। बीसवीं शताब्दी में औद्योगीकरण के आगमन से सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई। सामाजिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याओं ने विधिशास्त्रियों को इस ओर सोचने पर बाध्य किया कि सामाजिक समस्याओं के निवारण में विधि तथा विधिशास्त्रियों की क्या भूमिका होनी चाहिए।
उन्नीसवीं शताब्दी में राज्य के सम्बन्ध में अहस्तक्षेप (Laisses faire) का सिद्धान्त प्रचलित था। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का कार्य सिर्फ देश की सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था, मुद्रा संचरण तथा अन्य राष्ट्रों से सम्बन्धों के लिए कार्य करना है। राज्य को शिक्षा स्वरूप वाणिज्य (Commerce) तथा व्यापार (Trade) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए परन्तु बीसवों शताब्दी आते-आते अहस्तक्षेप के सिद्धान्त ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। अतः विधि के कार्यकलाप में बदलाव आया। राज्य ने अहस्तक्षेप के सिद्धान्त का अभित्यजन किया तथा कल्याणकारी (Welfare) सिद्धान्त को अपनाया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य ने जन-कल्याण के कार्यों में विशेष रुचि दिखाई। यह सिद्धान्त विकसित हुआ कि सामाजिक विषमता, समाज में व्यापार आर्थिक विषमता दूर करने के प्रयोजन से राज्य का हस्तक्षेप (laisses fair) का सिद्धान्त अब प्रासंगिक हो गया है। अब राज्य को कल्याणकारी (Welfarous) इकाई के रूप में कार्य करना होगा तथा राज्य के कल्याणकारी कार्यों को विधि द्वारा नियन्त्रित किया जाय, इसके लिए विधि को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक हुआ। यही कारण था कि विधि की समाजशास्त्रीय विचारधारा का उदय हुआ।
समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधिशास्त्रियों में काम्टे (A. Comte), हरबर्ट स्पेन्सर, रूडोल्फ वॉन इइरिंग, लीन डिग्यूट (ड्यूगिट), इंजी इहर्लिच (Engee Ehrlich), केन्रो रोविज (Herman Kanto Rowiez) गैर अमेरिकन विधिशास्त्री थे। दूसरी तरफ ओलिवर विन्डेल होम्स (Oliver Homes), बेन्जामोन मैथ्यू कार्डोजो (Benjamin Methew Cardozo) तथा रास्को पाउण्ड (Roscoe Pound) प्रमुख अमेरिकी समाजशास्त्रीय विधिशास्त्री हैं।
विधि की समाजशास्त्रीय विचारधारा के उद्गम के प्रमुख कारण –
(1) बीसवीं शतब्दी में व्यक्ति हित से सामाजिक हित पर विधिशास्त्रियों का ध्यान केन्द्रित हुआ।
(2) विधि की ऐतिहासिक विचारधारा, अधिनायकवादी आज्ञापक विचारधारा (Imperatical School) की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आयी। ऐतिहासिक’ विचारधारा ने विधि के निर्माण पर व्यक्ति की भूमिका को अस्वीकार किया तथा विधि को लोक चेतना (Volkgcist) का उत्पाद माना। ऐतिहासिक विचारधारा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि विधि तथा सामाजिक वातावरण जिनमें विधि विकसित होती है एक दूसरे से अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं। विधि की कल्पना समाज से हट कर अकेले नहीं की जा सकती। विधि के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है।
(3) उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित अहस्तक्षेप (laisses faire) के सिद्धान्त ने कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। उनके समाधान के लिए कल्याणकारी सिद्धान्त का विकास आवश्यक माना गया जिसमें सामाजिक समस्याओं के निवारण में विधि की भूमिका स्वीकार की गई। सामाजिक कार्यकलापों में विधि का हस्तक्षेप सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक माना गया।
(4) इस बात पर बल दिया जाने लगा कि विधि का अत्यधिक सैद्धान्तीकरण नहीं होना चाहिए, विधि को क्रियाशील (Active) होना चाहिए। विधिशास्त्रियों का कार्य विधि का औपचारिक विश्लेषण नहीं है परन्तु विधिशास्त्रियों को सामाजिक समस्याओं के निवारण के विषय में भी सोचना होगा।
(5) सामाजिक क्रान्ति तथा सामाजिक अव्यवस्था ने सामाजिक स्थिरता के बारे में आत्मसन्तुष्टि को विचलित किया तथा विधि की अक्षमता के बारे में चिंता को जागृत किया। सामाजिक विधिशास्त्री विधि की उस अक्षमता को दूर करना चाहते थे जिसके कारण सामाजिक समस्याएँ विकसित हो रही थीं। अब विधि (Law) को सामाजिक समस्याओं के निवारण का उपकरण या साधन माना जाने लगा ।
सामाजिक विचारधारा का विधिशास्त्र में योगदान – समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने विधिशास्त्र पर समाज के परिप्रेक्ष्य में विचार किया। इनके लिए विधि एक सामाजिक तथ्य है। विधिशास्त्र की कई विचारधारा के एकीकरण ने समाजशास्त्रीय विचारधारा को जन्म दिया। समाजशास्त्रीय विचारधारा के विधिज्ञ विधि को सामाजिक घटना (Social Phenominum) मानते हैं। विधि एक सामाजिक कार्य है। विधि, मानव समाज तथा मानव समाज के (व्यक्तिगत) सदस्यों से सम्बन्धित बाह्य सन्बन्धों से सन्दर्भित मानव समाज की अभिव्यक्ति है (Law is Expression of Human Society concerning the external relations of its individual members) समाजशास्त्रियों के अनुसार विधि को अपना ध्यान व्यक्तिगत हितों पर केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु विधि को सामाजिक उद्देश्य तथा विधि जिन हितों के लिए बनी है उस पर विचार करना चाहिए। विधि की चिता व्यक्तिगत हित न होकर सामाजिक हित के लिए होनी चाहिए। समाजशास्त्रीय विधिशास्त्री व्यापक रूप से तथ्यों तथा सामाजिक समूहों के विषय में व्यापक सम्भव अन्वेषण करते हैं जिससे कि विधि के निकायों के लिए और अधिक स्वास्थ्यकर वैज्ञानिक सिद्धान्त विकसित हो सके।
फ्रेन्च दार्शनिक मान्टेस्क्यू (1689-1755) विधिशास्त्र में सामाजिक तरीकों का अगुआ है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने विधिक प्रक्रिया पर सामाजिक स्थितियों के प्रभाव को मान्यता दी। उसके अनुसार विधि प्रत्येक राष्ट्र के लक्षणों के अनुरूप होनी चाहिए। विधि उस देश के लोगों, उस देश के वातावरण, उस देश की भूमि की गुणवत्ता, उस देश के लोगों के व्यवसाय के अनुसार सुनिश्चित होनी चाहिए। विधि के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अन्य स्वतन्त्रता तथा अधिकार किस सीमा तक दिया जाना चाहिए, उसका निर्धारण उनके समाज तथा उनकी प्रथा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मान्टेस्क्यू की प्रसिद्ध कृति थी ‘Spirit of Law’ (विधि की चेतना)।
एक फ्रेंच विधिशास्त्री ऑगस्ट काम्टे (1786-1857) को समाजशास्त्र के विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। कॉम्टे के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन का विधिक उद्देश्य समाज है न कि सरकार का कोई विशिष्ट निकाय। काम्टे के अनुसर विधि तथा सरकार की स्थापना करने के लिए आवश्यक प्रेरणा व्यक्तियों में उत्पन्न न होकर सामाजिक समूहों में उत्पन्न हुई है तथा व्यक्ति सदैव सामाजिक समूहों से जुड़ा रहा है।
इहरिंग (lhering) एक जर्मन विधिशास्त्री था। उसका पूरा नाम रूडोल्फ वोन इहंरिंग था। इसका जन्म ईस्ट फ्रिस्लैण्ड में औरिच (at Aurich) में 1818 में हुआ था। वह रोमन विधि का अध्यापक था। उसने अपना ग्रन्थ 1852 से 1865 तक चार खण्डों में प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ‘Spirit of roman law in various stages of development’ विकास के विभिन्न स्तरों में ‘रोमन विधि की चेतना’ 1867 में इहरिंग वियेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया।
इहरिंग के समय तक विधि अमूर्त अधिकारों (Abstract rights) को सीमित करने की पद्धति मानी जाती थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘Spirit of Roman Law’ में इहरिंग ने कहा कि विधि के स्रोत का उद्गम सामाजिक संघर्ष में है। अपने कार्यकाल के प्रारम्भिक दिनों में इहरिंग जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा को मानता था। इस दौरान उसने रोमन विधि का गहन अध्ययन किया। अपनी कृति में इहरिंग ने यह प्रदर्शित किया कि विधि की उत्पत्ति के लिए सामाजिक कारक उत्तरदायी थे। इहरिंग को समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। वह एक सामाजिक उपयोगितावादी (Social Utilitarian) था।
इहरिंग के अनुसार समाज में व्यक्तिगत स्वार्थी हितों तथा सामाजिक हितों के मध्य अपरिहार्य संघर्ष चाहता रहता है। इन परस्पर हितों के मध्य तालमेल बैठाने के लिए विधि उपाय करती है। ये उपाय पुरस्कार तथा उत्पीड़न या दण्ड के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार विधि को एक ऐसी पद्धति या प्रणाली (System) की संज्ञा दी जा सकती है जो समाज के परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ में इहरिंग ने कहा कि अधिकार का आधार हित है (The basis of right is interest) उसके अनुसार किसी विधिक प्रणाली की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के स्वार्थी, व्यक्तिगत हित तथा सामूहिक सामाजिक हित के मध्य तालमेल या सन्तुलन किस सीमा तक बैठाने में सफल या असफल है। समाज के हितों की रक्षा करन विधि का मूल पहलू (Basic aspect) है। विधि का उद्देश्य सामाजिक हितों को प्राप् करना, सामाजिक हितों की रक्षा करना, सामाजिक हितों का संवर्धन (Promotion) करना य सामाजिक हितों की सन्तुष्टि करना है।
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इहरिंग के अनुसार विधियाँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती हैं। विधि का लक्ष्य है सामाजिक नियन्त्रण का उपाय करना। विधि एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य है समाज के परस्पर विरोधी हितों के मध्य तालमेल स्थापित करना।
यूगेन इहरलिच (Eugen Ehrlich)- इहरिंग की जीवंत विधि की पुकार को उसके शिष्य यूगेन इहरलिच ने अपनाया। यूगेन इंहरलिच का जन्म 1862 में आस्ट्रोहंगेरियन साम्राज्य के एक हिस्से डच बुकोविना (Bukowina) के पास जनोंविट्ज (Zemowitz) में हुआ था वह जर्नीविट्ज में रोमन विधि का प्रोफेसर हो गया। सैविनी का मानना था कि विधि लोगों के प्राथमिक सज्ञानता के साथ जुड़ी रहती है जबकि यूगेन इहरलिच के अनुसार विधि समाज के वर्तमान निकायों (Present institution of society) में पाई जाती है। समाज की मूलभूत व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था जैसे विवाह, घरेलू सम्बन्ध, विरासत, कब्जा, संविदा आदि द्वारा शासित या नियन्त्रित होती है। इनके अनुसार विधि के वास्तविक स्रोत अधिनियम या निर्णीत वाद नहीं हैं। विधि का वास्तविक स्रोत समाज का क्रिया-कलाप है। उन्होंने निर्णय के मानक तथा ऐसे मानक जो समाज को नियन्त्रित करते हैं, में अन्तर किया। प्रत्येक विधि प्रणाली के औपचारिक नियम के मूल में एक सजीव तथा क्रियाशील विधि होती है। (At the root of every formal norm this is living and active Law)। इस प्रकार उन्होंने एक क्रियाशील विधि (Living Law) की वकालत की। क्रियाशील विधि को औपचारिक विधि में नहीं अपितु समाज में खोजा जाना चाहिए।
लियोन ड्यूगिट (Leon Duguit) (1859-1928) ड्यूगिट का सामाजिक समेकता (Social Solidarity) का सिद्धान्त – फ्रेंच विधिशास्त्री ड्यूगिट (Duguit) ने विधिशास्त्रीय समस्याओं को यथार्थवादी तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा। ड्यूगिट विश्लेषणात्मक विचारधारा को पूर्णरूप से अस्वीकार करता है। ड्यूगिट सम्प्रभु के विचार का पूर्णरूपेण खण्डन करता है। आधुनिक राज्य में विधि (Law in the modern state) में उसने विचार व्यक्त किया कि लोक सेवा के विचार ने सम्प्रभु के विचार को विस्थापित किया। अब राज्य समादेश निर्गत करने वाला सम्प्रभु शक्ति नहीं रह गया है। यह व्यक्तियों का समूह है, जिसे लोक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक राज्य के सिद्धान्त के आधार (मूल) में लोक सेवा (Public Service) का विचार होता है। सामाजिक जीवन के तथ्यों में लोक सेवा के विचार के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रहता।