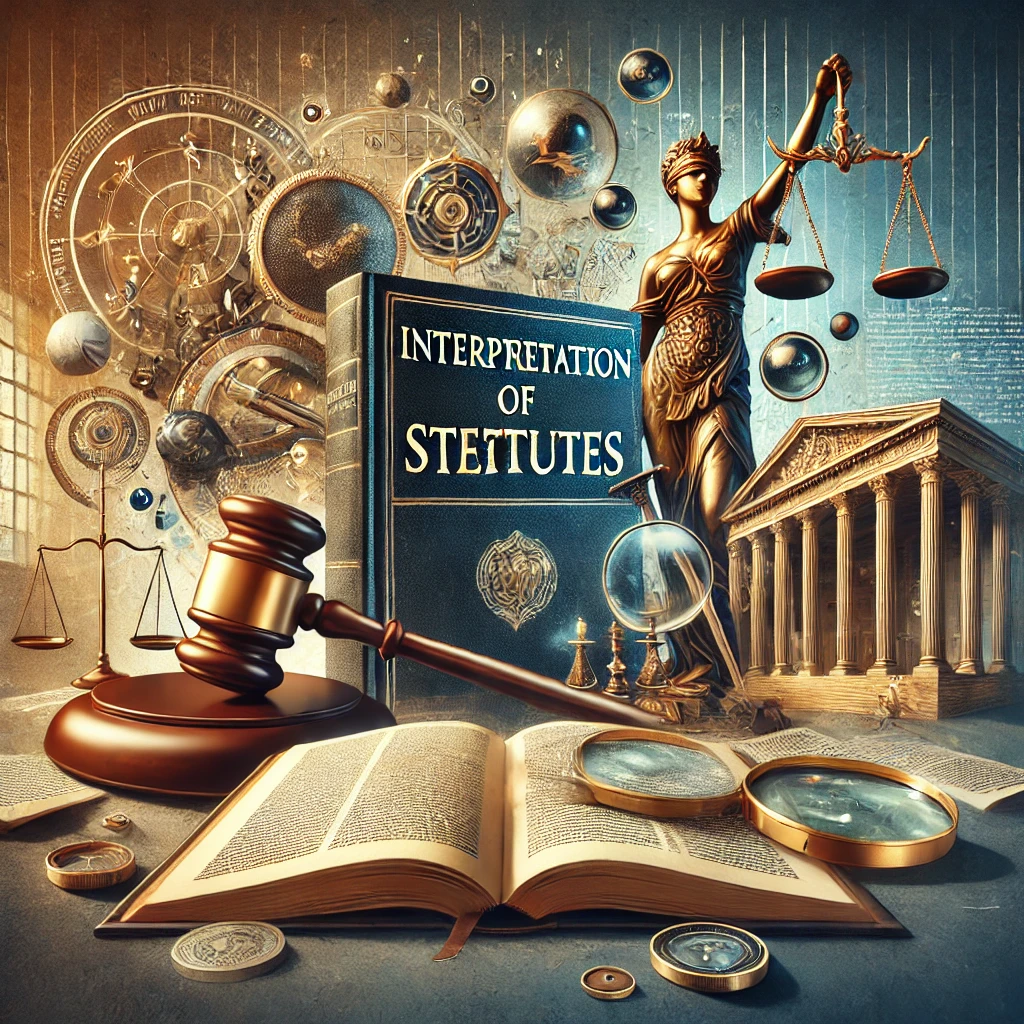-: लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
प्रश्न 1. कानून के निर्वचन से आप क्या समझते हैं? What do you understand by interpretation of statute.
उत्तर– कानून का निर्वचन (Interpretation of Statute ) — निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय संविधि के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। निर्वाचन का अर्थ है- अर्थ निर्धारण जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला आता है तो उस स्थिति में न्यायालय संविधि के रूप में अभिव्यक्त किये गये प्राधिकारिक सूत्रों को लागू करता है परन्तु जब इसे लागू करने में संदिग्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब न्यायालय निर्वाचन की सहायता से उस संदिग्धता को दूर करता है।
इस प्रकार विधायन के सही आशय को खोजने की इस पूरी प्रक्रिया को निर्वाचन के नाम से जाना जाता है।
सामण्ड महोदय के अनुसार, “निर्वाचन अथवा अर्थान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधान मण्डल का अर्थ उन माध्यमों द्वारा मालूम करते हैं जिन प्राधिकृत प्ररूपों के माध्यम से वह अभिव्यक्त किया गया है।”
ग्रे के अनुसार, “निर्वाचन एक विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किये गये शब्दों का वही अर्थ लगाया जाता है, जो विधायिका का आशय रहा हो या अनुमानतः आशय हो।
मैक्सवेल के अनुसार, “निर्वाचन वह पद्धति है जिसके द्वारा न्यायपालिका अधिनियम में प्रयोग किये गये शब्दों का अर्थ निर्धारित करती है।’
उपरोक्त परिभाषा के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधियों के निर्वाचन में न्यायाधीश संविधि के मूल आशय की खोज करता है फिर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है। इस तरह निर्वाचन मानव मस्तिष्क का कार्य है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
प्रश्न 2. संविधि से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Statute?
उत्तर- संविधि (Statute ) – सामान्यतः संविधि विधायिका को इच्छा है और विधायिका राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है जो जनता की इच्छाओं को विधायिका के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। विधायिका अपनी इच्छा को संविधि द्वारा क्रियान्वित करती है। मैक्सवेल के अनुसार, “संविधि विधायिका की इच्छा होती है” निर्वाचन में न्यायाधीश उसी इच्छा को लागू करने तथा संविधि की भाषा के संदिग्ध होने की स्थिति में उसके आशय को अन्वेषित करने का काम करता है। जब न्यायालय किसी संविधि की व्याख्या करता है तो निर्वाचन के नियम के अनुसार न्यायालय द्वारा जो भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है, वे संविधि के अंग बन जाते हैं।
प्रश्न 3. संविधि के निर्वाचन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। Discuss the purposes of interpretation of statutes.
उत्तर- संविधि के निर्वाचन के उद्देश्य (Purposes of Interpretation of Statutes) – निर्वाचन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मैक्सवेल महोदय ने अपनी पुस्तक “Interpretation of Statutes” में कहा कि “संविधियों के निर्वाचन का मुख्य उद्देश्य अथवा आशय यह निर्धारित करना है कि संविधि में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से क्या अर्थ है। इसमें यह भी देखा जाता है कि किसी वाद विशेष में व्याख्याकार द्वारा दी गयी व्याख्या प्रयोग होती है या नहीं।”
निर्वचन के प्रयुक्त उद्देश्यों में —
1. विधायिका में प्रयुक्त भाषा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या आशय है?
2. किसी वाद विशेष में व्याख्याकार की व्याख्या उपयोगी है या नहीं?
इस प्रकार जब उपरोक्त दोनों उद्देश्यों में समानता का अभाव पाया जाता है तब उसका निर्वाचन अनिवार्य हो जाता है। न्यायाधीशों द्वारा किया गया निर्वाचन का कार्य ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार एक स्वर्णकार किसी टूटे हुए आभूषण की मरम्मत कर उसे एक सूत्र में पिरोता है ठीक उसी प्रकार सम्पूर्ण संविधि के प्रावधानों का न्यायाधीश अर्थ निर्धारण करता है। आर० एम० डी० सी० बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1957) सु० को० 628 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि संविधि का निर्वाचन निर्माताओं के आशय के अनुरूप होना चाहिए।
अर्थात् निर्वचन का मुख्य उद्देश्य विधि-निर्माताओं के आशय को ढूँढ़ना है जिसके लिए विधायिका ने विवक्षित रूप से संविधि को शाब्दिक भाषा में कतिपय सुधार की शक्ति न्यायालयों को प्रत्यायोजित किया है बशर्ते कि ऐसा सुधार निष्पक्षता और न्याय प्राप्त करने के लिए जरूरी हो।
प्रश्न 4. निर्वाचन के (मूल) सामान्य नियम क्या हैं? What are basic rules of interpretation?
उत्तर- निर्वाचन मानव मस्तिष्क का कार्य है। निर्वाचन के नियम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि निर्वाचन न्यायालय का मनमाना कार्य है। निर्वचन करते समय भी न्यायालयों को कतिपय सुनिश्चित सिद्धान्तों तथा नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होता है जिन्हें हम मूल नियम के नाम से जानते हैं, इनमें से कुछ रोमन विधि के सूत्रों पर भी आधारित हैं, कुछ तर्क द्वारा रचित हैं तो कुछ विनिश्चयों में अधिकथित किये गये होते हैं।
ऐसे अनेक सामान्य नियमों में से कुछ नियम इस प्रकार हैं-
(1) विधि बनाने के सही आशय को सुनिश्चित करना चाहिए।
(2) विधि को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
(3) विधि को सन्दर्भ के साथ समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
(4) अमान्य से मान्य करना अच्छा है।
(5) सकारण लोप।
प्रश्न 5. निर्वाचन की शाब्दिक व्याख्या के नियम को समझाइये। Explain the literal rule of interpretation.
or
व्याकरणमूलक व्याख्या क्या है? What is grammatical interpretation?
उत्तर- शाब्दिक निर्वाचन का अर्थ – निर्वाचन के नियम का प्रथम सिद्धान्त शाब्दिकः निर्वचन है। इस नियम के अनुसार किसी भी संविधि की शाब्दिक व्याख्या ज्यों की त्यों की जानी चाहिए तथा व्याकरण के नियमों से शब्दों के प्रयोग का जो अभिप्राय निकलता हो, उसी को ठीक माना जाना चाहिए ताकि शब्दों का सहज एवं स्वाभाविक अर्थ लगाया जा सके।
क्राफोर्ड बनाम स्पूनर, 1846 प्री० कोo 181 के मामले में लॉर्ड चांसलर विस्काउण्ट 0 हाल्डेन ने कहा कि ” प्राकृतिक अर्थ लगाने के अलावा अन्यत्र कहीं विचारण नहीं कर सकते जब तक सम्पूर्ण अधिनियम के अवलोकन के पश्चात् इसकी आवश्यकता का अनुभव न हो रहा हो।”
प्रश्न 6. “लिटेश लेजिस एवं लिटेरा स्कृप्टा” क्या है? What is “Litera Legis and Litera Scripta”?
उत्तर- शाब्दिक व्याख्या के सन्दर्भ में “लिटेरा लेजिस” एवं “लिटेरा स्कृप्टा” का महत्वपूर्ण स्थान है। लिटेरा लेजिस एवं लिटेरा स्कृप्टा का अर्थ है-” लिपिबद्ध किये गये वैध शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं। ” इसमें यह स्पष्ट है कि इस लिपिबद्ध विधि में परिवर्तन करना न्यायालय के एकाधिकार क्षेत्र में नहीं है। न्यायाधीश अपनी इच्छा से इन शब्दों की व्याख्या नहीं कर सकता।
‘लिटेरा लेजिस में विधि के शब्दों का सम्मान महत्वपूर्ण एवं सुरक्षित माना गया है। जमना प्रसाद बनाम स्टेट, 1959 ए० एल० जे० आर० 620 के मामले में यह कहा गया है। कि “विधि की ऐसी ठोस शब्दावली को ही उत्तम माना जाता है जिससे एक ही अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता हो।”
अतः उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि संविधियों की व्याख्या करते समय उसमें प्रयुक्त भाषा का शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए। अन्यथा अर्थ लगाने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यही लिटेर लेजिस अथवा लिटेरा स्कृप्टा का सिद्धान्त है।
प्रश्न 7. व्याख्या के स्वर्णिम नियम से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Golden Rule of Interpretation?
उत्तर– व्याख्या का स्वर्णिम नियम सर्वप्रथम किसी संविधि के शब्दों की व्याख्या शाब्दिक निर्वचन के द्वारा ही किया जाना चाहिए परन्तु जब किसी संविधि में लापरवाही के कारण कोई भाषा सम्बन्धी त्रुटि समाहित हो जाती है तथा शाब्दिक निर्वाचन के माध्यम से विधायिका का आशय तथा विधि की भावना को स्पष्ट करने में असफलता मिलने लगे तो शाब्दिक निर्वाचन में कुछ परिमार्जन करके अर्थान्वयन करना आवश्यक हो जाता है। परिमार्जन करके अर्थान्वयन करना ही स्वर्णिम नियम के नाम से जाना जाता है।
अतः यह शाब्दिक निर्वचन का परिमार्जित रूप है। ग्रे बनाम पियर्सन, (1857) 10 ई० आर० 1216 के मामले में लार्ड से लेडेल ने कहा कि “जब व्याकरणीय एवं सामान्य निर्वाचन के नियम समुचित अन्वयन की भूमिका निभाने में सफल होते हैं तो उसे हो सर्वप्रथम अपनाया जाता है किन्तु जब शाब्दिक निर्वचन से असुविधा, कष्ट, अन्याय, असंगति अस्पष्टता, संदिग्धता और निरर्थकता का खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो संविधि के उक्त दुष्परिणामों से बचने के लिए शाब्दिक व्याख्या से कुछ हटकर विधि की व्याख्या की जाती है। इसे ही व्याख्या का स्वर्णिम नियम कहा जाता है।
प्रश्न 8. काशस ओसिस का क्या अर्थ है? What is meaning of “Casus Omissus”?
उत्तर- लोप का सिद्धान्त (Casus Omissus) – दो शब्दों से मिल कर बना है। Casus और Omissus जिसमें Casus का अर्थ है ‘due care’ अर्थात् जो सावधानी बरतनी चाहिए और Orissus का अर्थ है ‘Omission’ अर्थात् भूल इस प्रकार Casus omissus का अर्थ है वह बिन्दु जो संविधि में अन्तर्निहित नहीं है या कुछ ऐसे बिन्दु जो संविधि में शामिल होने चाहिए थे उसका लोप कर दिया गया है। इसी स्थिति को हम काशस ओमिसम कहते हैं।
परन्तु इस सकारण लोप को दूर करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। यह अधिकार विधायिका को है। विधायिका का इस कमी की तरफ ध्यान प्रायः संविधियों का निर्वाचन करते समय हो जाता है जिसे विधायिका की एक भूल के रूप में मान लिया जाता है या फिर ऐसा लोप भाषा की कठिनता तथा दोषपूर्ण शब्दावली से उत्पन्न होता है। इन कमियों को न्यायाधीश ही दूर कर सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है।
प्रश्न 9. संहिताकारी कानून क्या है? What is Codifying Statute?
उत्तर- संहिताकारी कानून (Codifying Statute) सामान्यत: संहिताकरण का अर्थ है, विधियों को समेकित करके लिपिबद्ध करना ताकि उनमें विरोधाभास या पुनरावृत्तिः का दोष उत्पन्न न हो।
सामण्ड के अनुसार, “समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहा जाता है।” संहिताकरण से विधि में योजनाबद्ध तरीके से विकास करके निश्चितता, सरलता, स्थिरता और तर्क संगतता लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सहिताकरण किसी विधि को विस्तारपूर्वक उपबन्धित करती है।
क्रेज के अनुसार वे संविधियों जो केवल किसी विशिष्ट बिन्दु पर विधि घोषित नहीं करतीं बल्कि किसी विशिष्ट विषय के बारे में सम्पूर्ण विधि को संहिता के माध्यम से घोषित करती हैं. संहिता कारक संविधियों है।
प्रश्न 10. निर्वाचन के तीन नियम क्या हैं? What are three rules of Interpretation?
उत्तर- सांविधिक निर्वाचन के तीनों नियम क्रमशः निम्न है-
(1) शाब्दिक नियम
(2) स्वर्णिम नियम
(3) दोष परिहार
प्रश्न 11. एजुडेम जेनेरिस ( सजातीय अर्थान्वयन) के नियम का क्या अर्थ है ? What is the meaning of the rule of Ejusdem generis?
उत्तर- एजुडेम जेनेरिस का अर्थ है- उसी प्रकार का अर्थात् इससे एक ही जाति का बोध होता है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ किसी भाषा में विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के पीछे सामान्य शब्दों को लिखा गया हो तो उन सामान्य शब्दों की व्याख्या विशिष्ट शब्दों के तादात्म्य में की जाएगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामान्य शब्द जो सामान्य प्रकृति के विशिष्ट शब्दों के बाद प्रयुक्त होते हैं वे अपना अर्थ विशिष्ट शब्दों से प्राप्त करते हैं।
यह नियम कोई विधि का सिद्धान्त नहीं बल्कि व्याख्या का एक नियम है जो विधायिका को मंशा को समझने में सहायता करता है जहाँ वह स्वयं में स्पष्ट नहीं है तो विशिष्ट शब्दों के साथ उसका अर्थ लगाया जाता है इसे हो सजाति का नियम कहा जाता है। जैसे-ब्रेड, बटर एवं अन्य यहाँ अन्य का अर्थ सजाति के नियम के अनुसार ब्रेड, बटर अर्थात् खाने-पीने की 1 वस्तुओं से ही लगाया जाएगा।
प्रश्न 12. साहचर्येण जायते का क्या अर्थ है? What is the meaning of ‘Noscitur a Socils?
उत्तर- साहचर्येण ज्ञायते (Noscitur a Sociis) — यह नियम दो शब्दों से मिल कर बना है- Noscitur और Sociis Noscitur का अर्थ है जानना तथा Sociis का अर्थ है साहचर्य अर्थात् शब्दों के अर्थ को उनके साहचर्य से जानना। दूसरे शब्दों में जब अर्थान्वयन में दो शब्दों का अर्थ एक-दूसरे के सम्पर्क में आने से दोनों का अर्थ यदि एक जैसा ही निकल रहा हो तो दोनों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए।
मैक्सवेल के अनुसार, साहचर्येण ज्ञायते का अर्थ है- जब दो या दो से अधिक शब्द जिनके समान अर्थ हो सकते हैं एक साथ दिये गये हों तो साहचर्य से उनका अर्थ लगाया जाएगा। वे अपने सजातीय अर्थ में प्रयुक्त किये गये समझे जाते हैं। वे अपना अर्थ एक दूसरे से ग्रहण करते हैं और अधिक सामान्य का अर्थ कम सामान्य के समान अर्थ तक कर दिया जाता है। अतः दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़े होने पर उसका अर्थ अधिक सामान्य को कम सामान्य से जोड़ कर निकाला जाएगा या फिर संदिग्ध शब्द को उसके तुरन्त नजदीक के शब्दों से जोड़ कर निकाला जाएगा।
प्रश्न 13. “एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है।” व्याख्या कीजिए। Explain the principle “Expressio unius est exclusio alterius”.
उत्तर-एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट इक्सक्लूजियो अल्टेरियस (Expressio unius est exclusio alterius)— इस सूत्र का तात्पर्य है-“एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है”। उदाहरण के लिए जहाँ किसी संविधि में किसी विशिष्ट श्रेणी की एक अथवा एकाधिक वस्तुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि उस संविधि से उस श्रेणी की अन्य वस्तुओं को अलग रखा गया है। मैक्सवेल ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी विशिष्ट वर्ग की एक या अधिक वस्तुओं के उल्लेख से यह समझा जा सकता है कि उस वर्ग की अन्य सभी वस्तुओं को चुपचाप अपवर्जित कर दिया गया है।
खेमका एण्ड कम्पनी बनाम महाराष्ट्र, राज्य, ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1549 में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (2) का अर्थान्वयन अन्तर्वलित था धारा 9 (2) के प्रथम भाग में केन्द्र और राज्य के प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण एवं दण्ड सम्बन्धी प्रावधान या पश्चातुवर्ती भाग में दण्ड केन्द्रीय विधान के सम्बन्ध में था। उच्चतम न्यायालय ने एक वस्तु का वर्णन दूसरे का अपवर्जन है, नामक सिद्धान्त लागू कर धारा 9 (2) के बाद वाले हिस्से में वर्णित दण्ड को केन्द्रीय अधिनियम के विशेष शक्ति वाले उपबन्धों तक ही सीमित रखा।
प्रश्न 14. तार्किक व्याख्या के नियम से क्या तात्पर्य है? What is meant by the rule of logical interpretation?
उत्तर – तार्किक व्याख्या– जहाँ संविधि में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तथा उससे विधायिका का अर्थ स्पष्ट न हो रहा हो तो वहाँ आशय स्पष्ट करने के लिए संविधि के उद्देश्य, कारण एवं कथन को देखा जा सकता है। यही “तार्किक व्याख्या” है। इसे “व्याख्या का उदार सिद्धान्त” (Doctrine of Liberal Interpretation) या ‘मेण्टेनसिया लेजिस’ (Sentential legis) “मेन्स” (mens) या सामाजिक या ऐतिहासिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है।
सामण्ड के अनुसार, “न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि संविधियों की व्याख्या करते समय वे विधायिका के आशय का पता लगायें तथा आशय के अनुरूप शब्दों का अर्थ निर्धारण करें।” इस प्रकार तार्किक व्याख्या का मुख्य उद्देश्य यही है कि संविधि की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि उससे विधायिका का आशय स्पष्ट हो जाए। तार्किक व्याख्या के अपने कुछ नियम भी हैं जो निम्न हैं-
1. संविधि को एक साथ पढ़ा जाना,
2. उपबन्धों की व्याख्या अलग-अलग नहीं किया जाना,
3. असंगतता को दूर करना.
4. परिणामों पर विचार नहीं करना,
5. तार्किक अर्थान्वयन किया जाना,
6. हितकारी अर्थान्वयन किया जाना,
7. विधायिका गलती नहीं करती। 1
प्रश्न 15. रिष्टि का नियम क्या है? What is Mischief Rule?
उत्तर- रिष्टि (Mischief) – रिष्टि का तात्पर्य है किसी को आशय के साथ क्षति या नुकसान पहुँचाना। जब कि व्याख्या के सन्दर्भ में रिष्टि के नियम का तात्पर्य है किसी संविधि के उपबन्धों के दुरुपयोग को रोकना।
पाण्डुरंग डगडूपास्ते बनाम रामचन्द्र बाबूराव हार्वे, ए० आई० आर० 1997 बम्बई 397 के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि “उत्तम यही है कि संविधियों की शाब्दिक एवं व्याकरणमूलक व्याख्या की जाये ताकि उसमें रिष्टि को स्थान न मिल पाये। यही एकमात्र ऐसी व्याख्या है जो अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य तक पहुँचा सकती है। “
उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि संविधियों की व्याख्या में रिष्टि (Mischief) का कोई स्थान नहीं है। अतः संविधियों की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें रिष्टि को स्थान न मिले सके मैक्सवेल ने भी कहा कि “संविधियों को व्याख्या के सन्दर्भ में न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे व्याख्या इस प्रकार करें कि उसमें रिष्टि का प्रवेश न होने पाये।
प्रश्न 16. दाण्डिक संविधियों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। How are Penal Statutes interpreted? Discuss with illustrations.
उत्तर- दाण्डिक संविधियों का निर्वचन – दाण्डिक संविधियाँ ऐसी संविधियाँ होती. हूँ जो राज्य के प्रति किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में दण्ड का प्रावधान करती हैं जिसमें राज्य एक पक्षकार होता है तथा अपराधी को ऐसे अपराध के सम्बन्ध में निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जाता है। दाण्डिक संविधियों के चार मुख्य नियम हैं जिनकी सहायता से दाण्डिक प्रावधानों का अर्थान्वयन किया जाता है—
(1) जब कोई संविधि किसी वर्ग-विशेष, कार्य-विशेष के सन्दर्भ में बनायी जाती है। तो वह उसी के ऊपर लागू होती है उसे खींचतान कर अन्य के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा।
(2) यदि संविधि का दो अर्थान्वयन संभव हो तो वही अर्थ देना चाहिए जो उपयुक्त हो, संदेह लाभ देता हो अर्थात् उसका संकुचित निर्वचन करना चाहिए।
(3) जब संविधि के शब्दों को व्यापक अर्थ दिया जाय यह अर्थ संविधि के आशय के अनुरूप हो तो वहाँ व्यापक अर्थ ही दिया जाना चाहिए।
(4) संविधि के किसी शब्द के अर्थान्वयन से कोई अन्य परिणाम निकल रहे हों तथा पूरी संविधि को एक साथ पढ़ने से ठीक अर्थ हो तो इस बेतुकापन (Absurdity) से बचने के लिए पूरी संविधि एक साथ पढ़ना चाहिए।
प्रश्न 17. हेडेन के नियम से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Heydon’s Rule’?
उत्तर – व्याख्या के इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी के अन्त में सन् 1584 में चान्सरी कोर्ट द्वारा हेडेन के वाद (Heydon’s Case) में प्रतिपादित किया गया था। इसीलिए इसे हेडेन के बाद के नाम से जाना जाता है, इसे अनिष्ट (दोष) परिहार नियम तथा रिष्टि के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
इस नियम का उद्देश्य संविधि में व्याप्त दोषों को दूर करने का और उसके लिए कोई उपचार प्रदान करने का है।
प्रो० डायसी का कहना है कि, “संविधि की शाब्दिक एवं व्याकरणमूलक व्याख्या के नियम को रिष्टि के नियम द्वारा अतिक्रमित किया जा सकता है। न्यायाधीशों को संभवतया संविधि की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि उससे रिष्टि का निवारण हो सके तथा उपचार प्रदान करने में आसानी हो।”
प्रश्न 18. लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? What do you mean by Welfare State?
उत्तर- प्रारम्भ में राज्य का कार्य केवल प्रशासन की स्थापना था और यह प्रशासन केवल बाह्य आक्रमण से रक्षा करने तथा राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करता था परन्तु धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और राज्य का ध्यान लोक कल्याण पर भी दिया जाने लगा। काण्ट के अनुसार, “कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करे।’ इस प्रकार कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो कि राज्य के नागरिकों के उत्थान के लिए कार्य करता है। यह उत्थान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक होता है।
प्रश्न 19. प्रो-प्राइवेटो कोमोडो तथा प्रो-बोना पब्लिको से क्या तात्पर्य है? What is meant by Pro-Privato Commodo and Pro-Bono Publico?
उत्तर- प्रो-प्राइवेटो कोमोडो तथा प्रो-बोना पब्लिको नामक दोनों सूत्र रिष्टि के नियम से सम्बन्धित हैं-
(1) प्रो-प्राइवेटो कोमोडो, तथा
(2) प्रो-बोना पब्लिको ।
इस दोनों सूत्रों का अर्थ है कि न्यायालयों द्वारा संविधियों की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि उससे रिष्टि का निवारण हो तथा उपचार सामने आये साथ ही विधायिका के सही आशय का पता लग जाने से आगे के लिए रिष्टि पर रोक लग सके। उसे इस प्रकार का बल प्रदान किया जाना चाहिए कि उससे विधायिका का सही आशय सामने आ सके।
प्रश्न 20. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Harmonious Construction?
उत्तर- सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन संविधि के उपबन्धों का अर्थान्वयन करते समय जब दो उपबन्धों का विरोध होने लग जाय या फिर एक के निर्वाचन से दूसरे उपबन्ध का अस्तित्व समाप्त होने लगे तो वहाँ ऐसी विधि से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि वह विरोध समाप्त हो जाय। विरोधाभास को समाप्त करने के लिए अपनायी गयी विधि को ही सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के नाम से जाना जाता है। सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विधायिका के आशय को किस प्रकार खण्डित नहीं होने देना है।
प्रश्न 21. संविधियों के न्यायिक निर्वचन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। Explain the nature of Judicial Interpretation of Statutes.
उत्तर— संविधियों का न्यायिक निर्वचन वर्तमान समय में एक सृजनात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। न्यायाधीश निर्वचन के माध्यम से मात्र विधि की खोज कर उसकी घोषणा ही नहीं करते हैं वरन् निर्वचन के माध्यम से वे विधि का निर्माण भी करते हैं। समाज न्यायाधीशों से अपेक्षा करता है कि वे विवादों का निपटारा युक्तिसंगत तरीके से करें। इस युक्तिसंगत तरीके से विवादों का निपटारा करते समय न्यायाधीशों को सृजनात्मक भूमिका निभानी पड़ती है। न्यायिक निर्णय निर्माण का अध्ययन जिसे निर्णय की प्रक्रिया कहा जाता है। न्यायिक प्रक्रिया में औचित्य के तर्क कौशल और निर्माण की प्रक्रिया दोनों का महत्व होता है।
प्रश्न 22. हितप्रद अर्थान्वयन क्या है? What is Beneficial Construction?
उत्तर- हितप्रद अर्थान्वयन (Beneficial Construction) — जब कोई उपचारी विधिक प्रावधान किसी वर्ग हित के लिए उपबन्धित किया गया हो तो वह हित उस व्यक्ति या वर्ग को दिया जाना चाहिए यदि शब्दों के प्राकृतिक अर्थ उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल होते हों तब उनका अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उस विधायन का आशय नष्ट न हो। ऐसी विधि को हितप्रद अर्थान्वयन के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 23. कर कानूनों के निर्वाचन के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। Explain the principle of Interpretation of Taxing Statutes.
उत्तर—कर संविधियों का निर्वाचन– लोक कल्याणकारी राज्य में जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए जनता पर कुछ कर प्रदान करने का कर्तव्य आरोपित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह स्वयंहित के बारे में सोचे व निर्धारित किये गये कर का संदाय करे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत Panzy Fernandez v. M. F. Queves. ए० आई० आर० 1963 इलाहाबाद 159 के मामले में करारोपण सम्बन्धी विधि की व्याख्या के तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं-
(1) कराधान विधियों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।
(2) विधि व्यवस्था के अनुसार ही कर संदाय के लिए विवश किया जाना चाहिए।
(3) संदेहास्पद स्थितियों की व्याख्या लोकहित में करना चाहिए।
अतः कराधान सम्बन्धी विधियों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि लोग कर से बच निकलें।
अनादि वेंकटेश्वरलू बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 945 के मामले में ‘चावल’ शब्द की व्याख्या का प्रश्न था कि क्या ‘चिवड़ा’ और ‘मुरमुरा’ भी चावल के रूप में हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक अर्थों में इन दोनों को चावल का ही रूप मानते हुए कहा कि चिवड़ा अथवा मुरमुरा को चावल का बदला हुआ रूप मानकर उस पर दुबारा कर अधिरोपित करना उचित नहीं है।
प्रश्न 24. पार्श्व टिप्पणी से क्या तात्पर्य है? What is meant by Marginal Note?
उत्तर- पाश्र्व टिप्पणी (Marginal Note) पार्श्व टिप्पणी धाराओं के बगल में लिखी होती हैं यद्यपि निर्वचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती क्योंकि पार्श्व टिप्पणी के महत्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका कारण यह है कि-
1. पार्श्व टिप्पणी संविधि का भाग नहीं होती,
2. इनका निर्धारण विधायिका द्वारा नहीं किया जाता है,
3. प्रायः ये अशुद्ध होती हैं।
परन्तु जब विधायिका द्वारा पार्श्व टिप्पणी जोड़ी गयी हो तब वह उस संविधि की व्याख्या में सहायक हो सकती है इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत का संविधान है।
पाश्र्व टिप्पण का प्रयोग तभी होगा जब संविधि की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध होने के कारण कोई निश्चित अर्थ न दे रही हो (एस० पी० गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, ए० आई० आर० 1982 एस० सी० 149 )