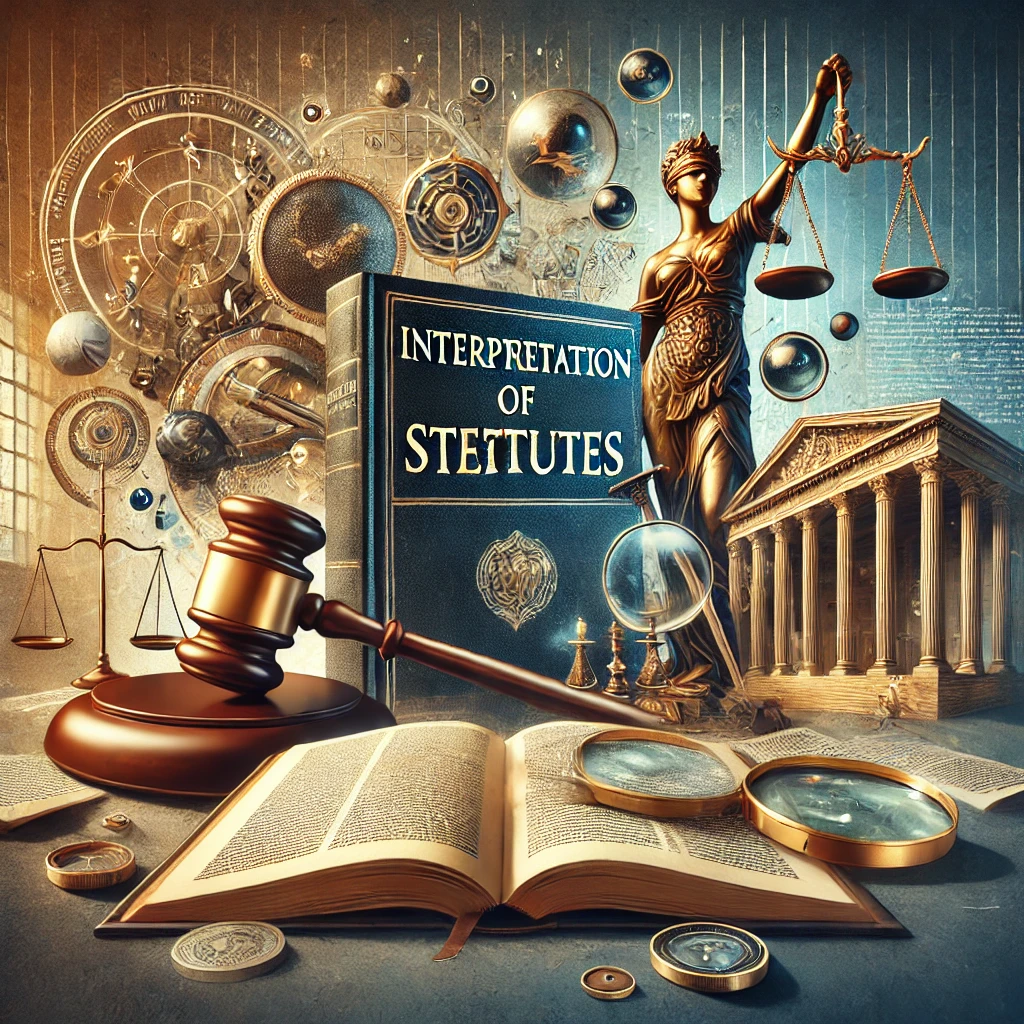-: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-
प्रश्न 1. संविधियों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं? निर्वचन का क्या उद्देश्य है, विवेचना कीजिए?
अथवा
संविधियों के निर्वाचन के अर्थ, उद्देश्य व क्षेत्र की विवेचना कीजिए?
अथवा
निर्वचन के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके उद्देश्य और प्रकार की विवेचना कीजिए।
What do you understand by Interpretation of Statutes. What is the object of such Interpretation of a Statute? Explain?
Or
Discuss the meaning, object and scope of Interpretation of Statutes.
Or
What do you know by Interpretation? Explain its object and types.
उत्तर- संविधि क्या है? – सामान्य रूप से संविधि विधायिका की इच्छा होती है और विधायिका राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है जो जनता की इच्छाओं को विधायन के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। विधायिका अपनी इच्छा को संविधि द्वारा क्रियान्वित करती है मैक्सवेल के अनुसार, संविधि विधायिका की इच्छा होती है और निर्वाचन में न्यायाधीश उसी इच्छा को लागू करने तथा संविधि की भाषा को संदिग्ध होने की स्थिति में उसके आशय को अन्वेषित करने का कार्य करता है तो निर्वाचन के नियम के अनुसार न्यायालय द्वारा जो भी प्रतिपादित किये जाते हैं, वे भी संविधि के अंग बन जाते हैं।
भारतीय संविधि का निर्माण केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायन द्वारा बनाया जाता है जिसे अधिनियमित विधि के नाम से जाना जाता है।
संविधि के निर्वचन का अर्थ –निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से न्यायालय संविधि के अर्थ को अभिव्यक्त करता है, निर्वचन का अर्थ है- अर्थ निर्धारण। जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला आता है तो उस स्थिति में न्यायालय संविधि के रूप में अभिव्यक्त किये गये प्राधिकारिक सूत्रों को लागू करती है परन्तु जब इसे लागू करने में संदिग्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब न्यायालय निर्वाचन की सहायता से उस संदिग्धता को दूर करता है।
इस प्रकार विधायन के सही आशय को खोजने की इस पूरी प्रक्रिया को निर्वाचन के नाम से जाना जाता है।
सामण्ड महोदय के अनुसार, “निर्वाचन अथवा अर्थान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधान मण्डल का अर्थ उन माध्यमों द्वारा मालूम करते हैं जिन प्राधिकृत प्ररूपों के माध्यम से वह अभिव्यक्त किया गया है।”
ग्रे के अनुसार “निर्वचन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अधिनियम में प्रयोग किये गए शब्दों का सही अर्थ लगाया जाता है, जो विधायिका का आशय रहा हो या अनुमानतः आशय हो।”
मैक्सवेल के अनुसार “निर्वाचन वह पद्धति है जिसके द्वारा न्यायपालिका अधिनियम में प्रयोग किये गये शब्दों का अर्थ निर्धारित करती है।”
उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधियों के निर्वचन में न्यायाधीश संविधि के मूल आशय की खोज करता है फिर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है। इस तरह निर्वाचन मानव मस्तिष्क का कार्य है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
प्रत्येक संविधि विधान मण्डल की इच्छा की मानसिक दशा होती है तथा वही आशय ही देश की सर्वोत्तम विधि कहलाता है।
जब विधायिका द्वारा किसी विवादास्पद संविधि की रचना की जाती है या संदिग्ध शब्दों की समुचित व्याख्या वह नहीं कर पाती तो इसके सही अर्थ के निरूपण के लिए न्यायाधीश को सृजनात्मक भूमिका निभानी पड़ती है। इस अर्थ निरूपण में न्यायालय सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों की सहायता लेकर संविधि को उसके उद्देश्य तक पहुँचाता है।
कोई संविधि बिना उद्देश्य के निरर्थक होती है इसलिए न्यायाधीश प्रत्येक संविधि में सन्निहित मूल आशय को खोजता है और उसका निर्वाचन की कसौटी पर परीक्षण करता है। इसके लिए वह निर्वचन के अनेक नियमों का सहारा ले सकता है।
निर्वाचन का उद्देश्य- संविधियों के निर्वचन का कार्य प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। परन्तु आज की अपेक्षा प्रारम्भ में उसकी उतनी महत्ता नहीं थी। निर्वाचन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए-
मैक्सवेल महोदय ने अपनी पुस्तक Interpretation of Statutes में कहा कि. ‘संविधियों के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य अथवा आशय यह निर्धारित करना है कि संविधि में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से क्या अर्थ है। इसमें यह भी देखा जाता है कि किसी वाद विशेष में व्याख्याकार द्वारा दी गयी व्याख्या प्रयोग होती है या नहीं। “
निर्वाचन के प्रमुख उद्देश्यों में
(i) विधायिका में प्रयुक्त भाषा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या आशय है?
(ii) किसी वाद विशेष में व्याख्याकार की व्याख्या उपयोगी है या नहीं?
इस प्रकार जब उपरोक्त दोनों उद्देश्यों में समानता का अभाव पाया जाता है तब उसका निर्वाचन अनिवार्य हो जाता है। न्यायाधीशों द्वारा किया गया निर्वचन का कार्य ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार एक स्वर्णकार किसी टूटे हुए आभूषण की मरम्मत करके उसे एक सूत्र में पिरोता है, ठीक उसी प्रकार सम्पूर्ण संविधि के प्रावधानों का न्यायाधीश अर्थ निर्धारण करता है। आर० एम० डी० सी० बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1957) सु० को० 628 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि संविधि का निर्वाचन निर्माताओं के आशय के अनुरूप होना चाहिए अर्थात् निर्वाचन का मुख्य उद्देश्य विधि- निर्माताओं के आशय को ढूंढ़ना है जिसके लिए विधायिका ने विवक्षित रूप से संविधि को शाब्दिक भाषा में कतिपय सुधार की शक्ति न्यायालयों को प्रत्यायोजित किया है बशर्ते कि ऐसा सुधार निष्पक्षता और न्याय प्राप्त करने के लिए जरूरी हो।
निर्वाचन के प्रकार– समय परिवर्तन के साथ ही निर्वाचन में भी अनेक नियम परिवर्तित होते रहते हैं परन्तु निर्वाचन के दो मूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं –
(1) व्याकरणमूलक या शाब्दिक व्याख्या;
(2) तार्किक व्याख्या।
(1) व्याकरणमूलक व्याख्या (Grammatical Interpretation) संविधियों की व्याख्या का प्रमुख नियम यह है कि किसी संविधि के शब्दों का अर्थान्वयन ज्यों का त्यों करना चाहिए तथा व्याकरण के नियमों से शब्दों का जो ठीक, सहज एवं स्वाभाविक अर्थ हो, लगाया जाना चाहिए। इससे सम्बन्धित एक सूत्र ‘Hitera Hagis या Hetare Scripta अर्थात् लिपिबद्ध किये हुए वैध शब्द ही विधि के परिचायक होते हैं। अतः न्यायाधीश निर्मित भाषा मैं कोई परिवर्तन एवं सुधार नहीं कर सकता। प्रथम नियम के अनुसार संविधि का आशय उसी में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से खोजा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में जब किसी विधि की शब्दावली स्पष्ट हो, साफ हो, तो उसे निर्वचन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्राफोर्ड बनाम स्पूनर, M.L.A. 1846 (4) 179 PC के मामले में प्रिवी कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम की संरचना अधिनियम के यथार्थ शब्दों के अनुसार की जानी चाहिए। हम यह नहीं ढूँढ़ सकते कि व्यवस्थापिका का क्या आशय यहाँ सम्भव रहा होगा, हम व्यवस्थापिका के अधिनियम के दोषपूर्ण वाक्य विन्यास में कुछ सहायता नहीं पहुँचा सकते और जो कमियाँ उसमें छूटी रह सकती हैं उसमें न तो कुछ जोड़ सकते हैं और न ही सुधार कर सकते हैं (सालोमन बनाम सालोमन एण्ड कम्पनी, ए० आई० आर०, 1987 एस० सी० 22)
(2) तार्किक व्याख्या (Logical Interpretation ) जब व्याकरणमूलक व्याख्या कोई अवांछित एवं असंगत परिणाम देने लगे तब संविधि के शब्दों की तार्किक व्याख्या की जाती है। दूसरे शब्दों में जहाँ संविधि में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तथा उससे विधायिका का अर्थ स्पष्ट न हो रहा हो तो वहाँ आशय स्पष्ट करने के लिए संविधि के.. उद्देश्य, कारण एवं कथन को देखा जा सकता है। एस० एस० बोला बनाम बी० डी० सरदाना, ए० आई० आर० 1997 एस० सी० 3127 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि –
‘जहाँ संविधि में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट एवं संदिग्ध हों तथा उनसे विधायिका का आशय प्रकट नहीं हो रहा हो, यहाँ विधायिका के आशय का पता लगाने के लिए संविधि के उद्देश्य, कारण कथन आदि पर विचार किया जा सकता है।”
निर्वाचन का क्षेत्र विस्तार – निर्वाचन का क्षेत्र विस्तार केवल अधिनियम या परिनियम ही नहीं बल्कि उसमें प्रयुक्त किये गये प्रत्येक शब्द एवं अभिव्यक्तियों को न्यायाधीश संदर्भित प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अवलोकित करता है तथा उसका कोई न कोई निर्णायक अर्थ भी ‘निकालता है। वर्तमान समय में व्यक्ति चारों तरफ से कानूनी जाल से घिरा हुआ है। कानून ही आज लोगों के संव्यवहारों, अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रति क्षण निर्धारण कर रहा है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलु को विधायन द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किया जाता रहा है क्योंकि लोक कल्याणकारी समाज में विधि जितनी ही अधिक होगी उतनी ही निर्वाचन को सम्भावनाएँ बहेंगी। अतः न्यायिक निर्वाचन का क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जाएगा।
इस प्रकार निर्वाचन एक सृजनात्मक कार्य है जिसका सहारा लेकर न्यायाधीश संविधि के आशय को अभिनिश्चित करता है। यह मानव मस्तिष्क का कार्य है इसीलिए इसमें ज्ञान विवेक, चिन्तन, आकलन एवं अनुसरण को प्रवृत्तियाँ निहित होती हैं।
प्रश्न 2. (i) संविधियों के निर्वाचन की न्यायिक प्रमाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
(ii) भारत में सांविधिक निर्वाचन में न्यायालयों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
(iii) सांविधिक निर्वाचन की सीमाएं क्या हैं? विवेचना कीजिए।
Write short notes on the Judicial Authority toInterpretation of Statutes?
Elucidate on the role of courts of the Statutory Interpretation in India.
What are the limitations of Statutory Interpretation? Explain.
उत्तर (i) – संविधियों के निर्वाचन की न्यायिक प्रमाणिकता (Judicial Authority to Interpretation of Statutes) संविधियों के निर्वाचन की प्रमुख प्रमाणिकता न्यायालयों को प्राप्त है। संसद की यह शक्ति प्राप्त है कि वह कॉमन लॉ अथवा पूर्व की किसी संविधि और सविधियों का निर्वाचन अथवा गलत निर्वाचन करने वाले न्यायिक विधानों को अस्वीकार्य घोषित कर दे अथवा निरस्त कर दे और घोषणात्मक अथवा निरसित करने वाली अधिनियमिति को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करें। गुजरात राज्य बनाम जीना भाई, (1972) के मामले में कृषि पद्धति के पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति पर विचार करते हुए न्यायाधीश आर० एस० सरकारिया ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विनिश्चय द्वारा विधान- मण्डल के आशय का सही निर्वाचन नहीं किया गया था तो संसद विधान द्वारा उसके प्रभाव को निराकृत कर सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि संसद न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधि के निर्वाचन भूतगामी प्रभाव वाली विधि का निर्माण कर अप्रभावकारी बना सकती है। परन्तु संसद द्वारा संविधि का इस तरह किया गया निर्वाचन अत्यन्त संकुचित होता है। संसद न्यायालय को गलत नहीं घोषित कर सकता है बल्कि उसके आधार को बदलकर उसे भूतगामी प्रभाव देकर अप्रभावकारी बना सकती है। संविधियों का निर्वाचन किस तरह किया जाय और संविधियों के निर्माण में न्यायाधीशों की क्या भूमिका हो इस सम्बन्ध में क्रेज ने अपनो कृति ‘स्टेट्यूट लो’ में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन करने का प्रयास किया है। सन् 1487 तक पॉलियमेष्ट रोल्स के आलोक में काउन्सिलर्स और ऑफिसियल्स के साथ-साथ न्यायाधीश भी लैटिन और नार्मल फ्रेंच में संविधि का प्रारूपण करते थे।
संविधियों के निर्वाचन की न्यायिक प्रमाणिकता अति प्राचीन है। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब जेम्स प्रथम ने सांविधिक निर्वाचन के अधिकार का दावा किया तो लॉर्ड कोक ने सभी न्यायाधीशों की सहमति से निर्णय सुनाया कि “विधायिका का दायरा अर्थान्वयन करना नहीं है बल्कि अधिनियमित करना है और उनके विचार जो घोषणात्मक उपबन्ध रूप में विधि के प्रारूप के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हैं, वह न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि न्यायालयों का कर्तव्य उनके द्वारा अधिनियमित संविधि की व्याख्या करना है ‘अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में मुख्य न्यायाधिपति आईयर ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि “संसदीय अधिनियमों की व्याख्या का अनन्य कर्तव्य राजा के लौकिक न्यायालयों और अन्तिम रूप में योर लॉर्डशिप्स के ऊपर न्यागत है।” विधिक इतिहास के किस मोड़ पर न्यायालय संविधियों का अनन्य प्रतिपादक बन गया, यह निश्चित करना सरल कार्य नहीं है। एक समय था जब विधायिका और न्यायालय की विभाजन रेखा स्पष्ट नहीं थी। यह भावना प्रबल थी कि संविधियों के निर्वचन का कार्य वही करें जिन्होंने उन्हें निर्मित किया है। यही कारण था कि मुख्य न्यायाधीश हेनधम ने विधि सलाहकार को झिड़कते हुए कहा था, “संविधि की अन्यथा व्याख्या न करो, क्योंकि हम लोग तुमसे बेहतर जानकारी रखते हैं, हम लोगों ने इसे बनाया है।” कतिपय मामलों में ऐसे भी दृष्टान्त मिलते। हैं कि हाउस ऑफ लाइस कठिन और महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के पूर्व संसद से परामर्श लेता था। धीरे-धीरे न्यायाधीशों को संसदीय कार्यवाही से अलग रखा जाने लगा। अन्तत: न्यायाधीशों के ऊपर संविधियों के निर्वचन का अनन्य भार आ गया। न्यायालय का कार्य विशिष्टतः विधि की शक्ति तथा इच्छा को प्रभावकारी बनाना माना गया। सन् 1824 में ओसबर्न बनाम बैंक ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जॉन मार्शल ने मत व्यक्त किया कि विधियों की शक्तियों से प्रति सुभेदक न्यायिक शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय विधि का उपकरण मात्र है और जो कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते, न्यायिक शक्ति का प्रयोग कभी भी न्यायाधीश की इच्छा को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता बल्कि हमेशा विधायिका की इच्छा अथवा दूसरे शब्दों में विधि की इच्छा को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। “मान्टेस्क्यू ने भी विचार व्यक्त किया था कि “राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश मात्र हैं जो विधि के शब्दों का उच्चारण करते हैं, निर्जीव वस्तु जो न तो इसके बल को अनुसीमित कर सकता है। और न ही इसकी दृढ़ता को न्यायालय ने संसदीय सर्वोच्चता के प्रादुर्भाव के बाद अपनी विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता बनाये रखने के लिए समय-समय पर यह भाव दर्शित किया कि वह संविधि का निर्वचन है और वह निर्वाचन के माध्यम से विधायिका के आशय को लागू करता है। संविधियों के न्यायिक निर्वचन की प्रमाणिकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि स्वयं विधि निर्माता इसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के बारे में बहुत निश्चित नहीं रहते हुए इसे इस आशा एवं विश्वास के साथ अधिनियमित करते हैं कि न्यायालय इसका प्राधिकारिक अर्थान्वयन कर इसे लागू करेगा।
न्यायालय की वस्तुपरकता एवं आत्मनियन्त्रण पूर्ण निर्वचन का परिणाम यह हुआ कि अब विधि की एक स्वयंसिद्धि (Axiom) स्वीकार्य हो गई है कि न्यायालय का केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है कि वह विधायी अधिनियमितियों के सन्देहपूर्ण उपबन्धों की व्याख्या एवं निर्वचन करे।
उत्तर (ii)- भारत में सांविधिक निर्वाचन में न्यायालयों की भूमिका – भारतीय विधिक व्यवस्था मूलतः आंग्ल विधि व्यवस्था पर आधारित है। संविधान लागू होने के दो दशकों में उच्चतम न्यायालय आंग्ल प्रमाणवादी विचारधारा से प्रभावित भी रहा। मैक हिनी ने अपनी कृति “जूडिशियल रिव्यू” में टिप्पणी की कि जब तक भारतीय विधिक शिक्षा आंग्ल प्रमाणवादी तरीके से बद्ध है और जब तक आंग्ल ट्रेनिंग के न्यायिक निर्णय देने वाले न्यायालय में है तब तक यन्त्रवत् प्रमाणवादी दृष्टिकोण ज्यादा सजग, उद्देश्यपूर्ण और नीति अभिमुख दृष्टिकोण पर हावी रहेगा। ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए० आई०. आर० (1950) सु० को 27 के मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का तात्पर्य मात्र विधायिका द्वारा स्थापित प्रक्रिया तक संकुचित कर अनुच्छेद 21 में दी गयी सुरक्षा को मात्र शब्दाडम्बर तक संकुचित कर दिया गया है।
परन्तु भारतीय विधिक व्यवस्था में इंग्लैण्ड की अपेक्षा अमेरिकन विधिक व्यवस्था द्वारा अपनाये गये निर्वाचन में न्यायालयों की भूमिका ज्यादा समीचीन साबित होगी। भारतीय सांविधिक निर्वाचन अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे परिसंघीय ढाँचे वाले लिखित संविधान द्वारा शासित देशों के सांविधिक निर्वाचनों के ज्यादा नजदीक होंगे। इंग्लैण्ड की तरह “विधि विधि है” की मानसिकता नहीं अपनायी जा सकती बल्कि विधि की अन्तर्वस्तु के आधार पर ही उसकी वैधानिकता आधारित होगी।
भारतीय न्यायालयों का एक पथ-प्रदर्शक आंग्ल व्यवस्था पर आधारित ज्यादा पाठ पर आधारित या शाब्दिक दृष्टिकोण नहीं होगा बल्कि अमेरिकन न्यायालयों का दृष्टिकोण होगा जो संविधि के ज्यादा उद्देश्यात्मक निर्वाचन की अपेक्षा रखेगा। भारतीय न्यायालयों के लिए सांविधिक निर्वाचन का आज्ञापक नमूना, जो इंग्लैण्ड में प्रचलित है, ग्राह्य नहीं होगा बल्कि निर्वचनात्मक नमूना ग्राह्य होगा जो संविधि को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करने को प्रेरित करेगा। यद्यपि कि भारतीय न्यायालय इस बात की स्पष्टतः स्वीकार नहीं कर रहे हैं फिर भी वे आज्ञापक प्रारूपिकता द्वारा उत्पन्न ब्रिटिश न्यायालयों की संकुचित विधि निर्माण की भूमिका के ढर्रे को छोड़कर मौलिक तर्कयुक्ति पर आधारित अमेरिकन न्यायालयों की विस्तृत विधि निर्माण प्रवृत्ति को अपनाये जा रहे हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय की सांविधिक निर्वाचन के सम्बन्ध में इस प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ।।
मेनका गाँधी बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1978) सु० को० 597 के निर्णय में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया के वैध होने के लिए आवश्यक होगा कि वह ऋजु युक्तियुक्त और न्यायपूर्ण हो तथा निरंकुशता से हीन हो।
भारत में उच्चतम न्यायालय के पास सर्वोपरि अवशिष्ट न्यायिक शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 142 में उपबन्धित किया गया है कि “उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लम्बित किसी बाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।”
यूनियन कारबाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1992) सु० को० 248 के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 142 में उपलब्ध शक्ति को अभिव्यक्त सांविधिक प्रतिषेध द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे उपबन्ध केवल किसी विशिष्ट मामले में इस शक्ति के प्रयोग की समीचीनता को प्रभावित कर सकते हैं।
काशीनाथ जी जाल्मी बनाम दी स्पीकर, (1993) 2 सु० को० के० 226 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्ति का विस्तार कर तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुकूल आदेश पारित करने की सामर्थ्य प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998) सु० को० के० 201 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 में प्राप्त असीमित शक्ति के ऊपर कतिपय नियन्त्रण स्वीकार किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि कि अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति को किसी तरह सांविधिक उपबन्ध द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है परन्तु साथ ही साथ इन शक्तियों का प्रयोग वहाँ अपेक्षित नहीं है जहाँ इसका प्रयोग किसी विषय से अभिव्यक्त रूप में सम्बन्धित संविधि के अभिव्यक्त उपबन्धों से वह सीधे अन्तर्विरोध में आता है।
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 सु० को० के० 201 के बाद में संविधान पीठ का 41 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश आर० सी० लाहोटी ने अभिमत व्यक्त किया कि संविधियों के निर्वाचन का अनन्य विशेषाधिकार सांविधिक न्यायालयों को है।
उत्तर (iii) सांविधिक निर्वाचन की सीमाएं – सांविधिक निर्वसन का उद्देश्य विधि में आवश्यक सुधार कर निष्पक्षता एवं न्याय को सुनिश्चित करना है। न्यायालय यह कार्य विधायिका का आशय ढूँढ़कर करता है। प्रो० हैराल्ड जे० लास्की के शब्दों में निर्वाचन की पद्धति का स्वरूप विश्लेषणात्मक कम किन्तु व्यावहारिक अधिक होना चाहिए, उसे विधायी विचारधारा के प्रभाव का पता लगाने वाला होना चाहिए जिससे उस सामाजिक मूल्य को जिसे प्राप्त करना आशयित है, पूरा बल प्रदान किया जा सके। परन्तु निर्वाचन की कतिपय सीमाएँ हैं। लॉर्ड डेनिग ने संविधि की कमियों एवं विसंगतियों को दूर करना निर्वचन में सम्मिलित माना परन्तु कहा कि न्यायाधीश को उस सामग्री में परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिस पर अधिनियम का ताना-बाना बुना गया है। कृष्ण गौड़ बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (1976) 3 उम० नि० प० 583 के बाद में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने स्पष्ट किया कि “विधि को पुनः रचना न्यायाधीश नहीं कर सकते चाहे नागरिकों के रूप में शीघ्र सुधार करने के लिए उनके मत वैसे भी क्यों न हो?
अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1969) 2 उम० नि० प० 253 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि यदि किसी अधिनियमिति की किसी धारा में कोई भूल हो गयी हो तो उसका सुधार विधामण्डल ही कर सकता है। निर्वाचन के माध्यम से न्यायालय द्वारा ऐसा करना अनुमत नहीं है।
काफोर्ड बनाम स्यूनर, 4 मू० सी० सी० सी० 187 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि “हम (न्यायालय) विधानमण्डल की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते और अर्थान्वयन कर उसकी कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं।
बंगलौर वाटर सप्लाई कम्पनी बनाम ए० राजप्पा, (1979) 2 उम० नि० प० 1053 के मामले में क्राउन द्वारा रचित कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू०) 31) को उद्धृत करते. हुए अभिनिर्धारित किया गया कि “न्यायालय विधायी निकाय के निर्णयों के स्थान पर अपनी सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट माइनिग ऑफिसर बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, (2001) ? सु० को० के० 538 के वाद में तीन सदस्यीय पीठ का निर्णय देते हुए न्यायाधीश जी० बी० पटनायक ने माइन्स एण्ड मिनरल्स सेस एण्ड अण्डर टैक्सेज ऑन मिनरल्स (वैलिडेशन ) ऐक्ट, 1992 के उपबन्धों की व्याख्या करते हुए कहा कि न्यायालय का कार्य केवल विधि का पता लगाना है, विधि का अधिनियमन करना नहीं।
भारत संघ बनाम राजीव कुमार, (2003) 6 सु० को० के० 516 के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 (2) मैं कतिपय शब्दों को जोड़कर 48 घण्टे से ज्यादा अवधि हेतु हिरासत में निरोध की दशा में सरकारी सेवक का निलम्बन मान लिए जाने को निरोध की अवधि तक निलम्बन को सीमित रखने की दलील को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश अरिजीत पसायत ने यह स्पष्ट किया कि एक उपबन्ध का निर्वचन करते समय न्यायालय केवल विधि का निर्वचन करता है। वह विधि निर्माण (विधायन) नहीं कर सकता है। यदि विधि के उपबन्ध का कोई दुरुपयोग हो रहा है तो यह विधायिका के लिए है कि वह यदि आवश्यक समझे तो उसे संशोधित या निरसित कर दे। न्यायालय विधायी सकारण लोप की आपूर्ति न्यायिक निर्वचनात्मक प्रक्रिया द्वारा नहीं कर सकते।
बेमारेण्डी कुमार स्वामी रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (2006) 2 सु० को० के० 670 के बाद में न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने अभिमत व्यक्त किया कि एक प्रावधान का निर्वचन करते समय न्यायालय मात्र विधि का निर्वचन करता है और उसका विधायन नहीं कर सकता है। यदि एक प्रावधान का दुरुपयोग होता है और विधि को प्रक्रिया दुरुपयोग के अधीन बनायी गयी है, तो आवश्यक समझने पर यह विधायिका के लिए है कि वह संशोधन, सुधार अथवा निरसन करे।
प्रश्न 3. “निर्वाचन एवं अर्थान्वयन के बीच की विभाजन रेखा अत्यन्त क्षीण है। व्याख्या कीजिए।
अथवा
“क्या निर्वाचन और अर्धान्वयन एक ही अर्थ के द्योतक हैं अथवा दोनों अलग-अलग भावों को अभिव्यक्त करते हैं।” व्याख्या कीजिए। “The dividing line between the interpretation and construction is very thin.” Explain.
उत्तर- सांविधिक विधि को प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्राधिकार नियमों को समाविष्ट करती है। जिन शब्दों में संविधि अभिव्यक्त होती है वे स्वयं विधि के भाग होते. हैं। संविधि के शब्दों एवं आत्मा (Spirit) दोनों में विधिक प्राधिकारिता पायी जाती है। यह लक्षण विधि के अन्य स्रोतों में नहीं पाया जाता। अतः अधिनियमित विधि के सम्बन्ध में संविधि के अर्थों की जानकारी आवश्यक बन जाती है। इस जानकारी के लिए दो भावार्थों का प्रयोग किया जाता है-
(1) निर्वाचन (Interpretation), और
(2) अर्थान्वयन (Construction) |
विधिशास्त्रियों के बीच इस बात पर मत वैभिन्य जारी है कि निर्वचन और अर्थान्वयन एक ही अर्थ के द्योतक हैं अथवा दोनों अलग-अलग भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस सम्बन्ध में तीन मत पाये जाते हैं-
(क) निर्वाचन एवं अर्थान्वयन एक हैं- विधि विशेषज्ञों द्वारा दोनों भावार्थों को एक- दूसरे का समानार्थी माना गया है। सामण्ड द्वारा निर्वाचन और अर्यान्वयन का प्रयोग एक-दूसरे के विकल्प के रूप में किया गया है। सामण्ड ने निर्वाचन अथवा अर्थान्वयन को एक प्रक्रिया माना जिसके द्वारा न्यायालय प्राधिकृत प्ररूपों के माध्यम से अभिव्यक्त विधान मण्डल का आशय ढूंढता है। क्राफोर्ड ने निर्वाचन और अर्थान्वयन को प्रक्रियाओं के बीच विभेद को अस्पष्ट मानते हुए कहा कि न्यायालयों के लिए इसका प्रकट रूप में अत्यन्त अल्प अथवा नहीं के बराबर महत्व है।
राजस्थान राज्य बनाम दी मेवाड़ सुगर मिल्स लिमिटेड, ए० आई० आर० 1969 सु० को० में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिसे निर्वचन कहा जाता है उसे अर्थान्वयन भी कहा जाता है और जिसे अर्थान्वियन कहा जाता है उसे निर्वाचन भी कहा जाता है।
(ख) निर्वाचन एवं अर्थान्वयन के बीच विभाजन रेखा क्षीण है- डायस ने ‘अर्थ’ और’ आशय’ की संदिग्धता के समाधान तथा शब्दों के अर्थ एवं उद्देश्य की खोज के लिए इन दोनों भावार्थों को सहायक माना है। डायस के अनुसार निर्वाचन मुख्यतः सांविधिक शब्दों के अर्थ से सम्बन्धित है, जबकि अर्थान्वयन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विधायिका का आशय निश्चित किया जाता है। परन्तु डायस नै विधिशास्त्र के पाँचवें संस्करण में यह उल्लेख किया है कि न्यायालय की गतिविधियों का इस तरह विभाजन नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि निर्वाचन एवं अर्थान्वयन के बीच स्पष्ट विभेद नहीं है। जहाँ भाषा अनेकार्थक अथवा सन्दिग्धार्थक (Equivocal) है, यह निर्णय कि भाषा न्यायालय के समक्ष उपस्थित स्थिति को निर्दिष्ट करती है, जिसे संविधि पारित करने के समय कोई सोच नहीं सकता था, अपरिहार्य रूप से अर्थान्वयन के अध्युपाय को आमन्त्रित करता है। डायस के अनुसार ऐसे मामलों में यह जान पाना कठिन है कि कहाँ निर्वाचन की सीमा समाप्त हो जाती. है और अर्थान्वयन की सीमा कहाँ प्रारम्भ होती है तथा डायस ने स्पष्ट किया कि विधायिका के उद्देश्य के निर्धारण हेतु न्यायालय की अधिनियमिति के बाहर जाकर नीति ढूँढने की अनुमति दी जा सकती है जिसके आलोक में शब्दों का अर्थान्वयन किया जा सके।
सर रूपर्ट क्रास ने ब्लैकस्टोन द्वारा संविधियों के अर्थान्वयन हेतु दिये गये दस नियमों का जिक्र करते हुए टिप्पणी की है कि निर्वाचन और अर्थान्वयन के बीच विभेद के लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है और न ही प्रत्येक शीर्षकों में वर्णित विषय सामग्री से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
(ग) निर्वचन और अर्थान्वयन दोनों अलग-अलग भावों को अभिव्यक्त करते हैं अर्थात् दोनों में भिन्नता – कुछ विधि विशेषज्ञों का मत है कि निर्वाचन एवं अर्थान्वयन के बीच विभेद सम्भव और वांछनीय दोनों हैं। एक में निर्वाचन की व्याख्या शब्दों के वास्तविक अर्थ ढूँढ़ने की कला के रूप में की जाती है। दूसरे में निर्वाचन शब्दों में विधायिका के आशयित भाव को ढूँढ़ता है और कुछ नहीं, दूसरी ओर अर्थान्वयन का तात्पर्य विधि की भावना (Spirit) में से अर्थ निकालना है, विधि के शब्दों में से नहीं। अर्थान्वयन का प्रयोग वहाँ ज्यादा समीचीन माना गया है जहाँ न्यायालय विशिष्ट रूप से प्रयुक्त शब्दों से अर्थ निकालने की अपेक्षा कुछ ज्यादा सृजनशील भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि डॉ० पैट्रिक ट्रेवलिन ने अर्थान्वयन को ज्यादा बेहतर शब्द माना है।
पैट्रिक डेवलिन के अनुसार यद्यपि कि अर्थान्वयन का प्रयोग प्रायः निर्वाचन के वैकल्पिक रूप में किया जाता है फिर भी अर्थान्वयन यह बतलाता है कि संविधि में प्रयुक्त शब्दों के संकुचित निर्वचन से उपलब्ध किये जाने के बजाय विषय-वस्तु के वर्णन से कुछ ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है। अथन्वियन पूर्ण भाव में विधि की ऐसी शाखा में अपने को व्यवस्थित करता है जिससे कि वे विधि को उस रूप में निर्मित कर सकें। धन कर आयुक्त बनाम हशमतुनिशा बेगम, ए० आई० आर० (1989) सु० को० 1024 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पैट्रिक डेवलिन के इस मत को उद्धृत किया गया है।
निर्वाचन संविधि के शब्दों द्वारा आशय ढूंढ़ता है जबकि अर्थान्वयन में सादृश्य के आधार पर तर्क युक्ति के निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने इनरी सी कस्टम्स ऐक्ट, ए० आई० आर० (1963) सु० को० 1760 के परामर्शदायी विचार में लिखित संविधान की व्याख्या के निर्वचन और अर्थान्वयन दोनों शास्त्रीय दृष्टिकोणों को स्पष्ट करते हुए कहा कि “लिखित संविधान में सर्वाधिक मामलों में कार्य निर्वचन करना होना चाहिए परन्तु जहाँ संविधान की भाषा इंगित करती है कि जो समानान्तर विषयों पर दूसरे देशों के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा पहले निर्णीत है उसे ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ पाठ के थोड़ा आगे जा कर निष्कर्ष ढूँढना होगा कि क्या प्राप्त करना है और क्या परिवर्तित करना अपेक्षित है।”
यद्यपि कि अधिकांशत: विधिशास्त्रियों एवं सांविधिक निर्वाचन पर पाठ्य पुस्तक लेखकों ने निर्वाचन एवं अर्थान्वयन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर किया है फिर भी इन दोनों भावार्थों में विभेद अब ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। वर्तमान समय में ब्रिटिश प्रमाणवादी विचारधारा के शाब्दिक निर्वाचन की परम्परा से आगे बढ़कर न्यायिक सृजनशीलता की अपेक्षा की जा रही है।
प्रश्न 4. संविधि से आप क्या समझते हैं? संविधियों के वर्गीकरण की सविस्तार व्याख्या कीजिए। What do you understand by statutes? Explain in detail the classification of statutes.
उत्तर- संविधि (Statutes) – संविधि विधायिका की इच्छा होती है और विधायिका राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है जो जनता की इच्छाओं को विधायिका के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। विधायिका अपनी इच्छा को संविधि द्वारा क्रियान्वित करती है।
मैक्सवेल के अनुसार, “संविधि विधायिका की इच्छा होती है। भारतीय संविधि का निर्माण केन्द्रीय या प्रान्तीय विधायन करती है जिसे अधिनियमित विधि के नाम से जाना जाता है।
व्यापक रूप से सामाजिक व्यवहारों को संचालित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विधि का उद्भव होता है। कुछ विद्वानों ने ऐसी विधियों को लिखित या अलिखित विधि की संज्ञा दी है। सम्प्रभु द्वारा भी प्रचलित विधियों को मान्यता प्रदान कर इस श्रेणी की वैधता प्रदान कर दी जाती है। सभी विधियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उपयोग मानवीय व्यवहारों में समीचीन होता है। इसके विकास का कारण चाहे हेनरीमैन की गतिशीलता हो या डीन रास्को पाउण्ड की सामाजिक अभियांत्रिकी विचारधारा हो निरन्तर प्रगतिशील है-
संविधियों के वर्गीकरण का आधार वर्तमान समय में विधायन द्वारा जितने प्रकार की विधियाँ समाज में विद्यमान है, उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से चार आधारों पर किया जा सकता है-
1. अवधि के सन्दर्भ में वर्गीकरण,
2. कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकरण,
3. उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण,
4. प्रवर्तन के आधार पर वर्गीकरण।
1. अवधि के आधार पर वर्गीकरण – अवधि के आधार पर संविधियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-
1. स्थायी विधि,
2. अस्थायी विधि।
स्थायी विधि – ऐसी विधियाँ जिनके संचालन के लिए कोई निर्दिष्ट समय नहीं दिया – जाता जब तक कि किसी दूसरे अधिनियम द्वारा संशोधित या परिवर्तित न किया जाये तब तक इनके विस्तार की अवधि विद्यमान रहती है इसे ही स्थायी विधि कहा जाता है जैसे – भारतीय संविदा विधि, साक्ष्य विधि, भारतीय दण्ड संहिता इत्यादि ।
अस्थायी विधि – ऐसी विधियाँ जिनके वैधता का काल विधि द्वारा स्वयं ही सुनिश्चित कर दिया जाता है यदि इसे निर्धारित अवधि के भीतर निरसित नहीं किया गया तो वह विधि अपनी निर्धारित अवधि तक बनी रहती है और अवधि के बीतने पर यदि उसकी आवश्यकता बनी रहे तो विधायिका उसका नवीनीकरण करती रहती है। ऐसी विधियों को अस्थायी विधि कहा जाता है। जैसे—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370, 349, 250, 252 इत्यादि ।
2. कार्य प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण – कार्य प्रणाली के आधार पर संविधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- (अ) आज्ञापक विधि या आदेशात्मक विधि, (ब) निदेशात्मक विधि।
(अ) आदेशात्मक विधि – यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें निश्चित कार्यों को निश्चित तरीके से करने की पूरी बाध्यता होती है। उदाहरण स्वरूप-व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार किसी भी वाद को वादपत्र द्वारा ही संस्थित किया जा सकता है। बिना वादपत्र के न्यायालय के समक्ष वाद की उपधारणा हो ही नहीं सकती है।
(ब) निदेशात्मक विधि- यह विधि मात्र यह निर्देश देती है कि किसी कार्य को किया जाये। यदि उस कार्य के या उसके प्रस्तावित ढंग का पालन न किया जाए तो ऐसा करना उसकी वैधता के लिए सदैव घातक नहीं होता।
3. उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण – उद्देश्य के आधार पर संविधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे आधारों पर विधि के सृजन से ले कर उसका प्रभाव तथा प्ररूप सब अन्तर्निहित होता है। इसके निम्न स्वरूप हैं-
1. संहिताकारी विधि (Codifying Statutes),
2. समेकनकारी संविधि (Consolidating Statutes),
3. घोषणात्मक संविधि (Declaratory Statutes),
4. उपचारी विधि (Remedial Statutes),
5. समर्थकारी संविधि (Enabling Statutes),
6- दण्ड संविधि (Penal Statutes ),