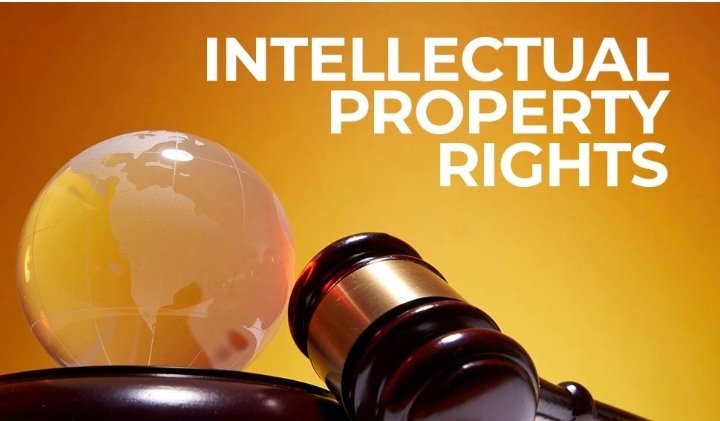प्रश्न 1: बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) का क्या मतलब है? इसके रूप और कानूनी दायरे का उल्लेख करें।
उत्तर:
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनकी मानसिक रचनाओं (जैसे- विचार, आविष्कार, डिज़ाइन, साहित्यिक कृतियाँ) पर मिलते हैं। यह अधिकार उन्हें अपनी रचनाओं का उपयोग, वितरण और पुनरुत्पादन करने का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। IPR के मुख्य रूप हैं:
- कॉपीराइट (Copyright): यह अधिकार लेखक, संगीतकार, कलाकार आदि को उनकी रचनाओं पर प्राप्त होते हैं।
- पेटेंट (Patent): यह आविष्कारक को उनके नए आविष्कार पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- ट्रेडमार्क (Trademark): यह किसी व्यवसाय या उत्पाद का विशिष्ट पहचान चिन्ह होता है, जो उसे अन्य से अलग करता है।
- डिजाइन (Design): यह उत्पाद की विशेष डिजाइन पर अधिकार होता है।
- गोपनीयता और व्यापार रहस्य (Trade Secret): किसी कंपनी की व्यापार रणनीतियाँ और जानकारी पर अधिकार।
- पौधों के किस्में (Plant Varieties): कृषि क्षेत्र में पौधों की नयी किस्मों पर अधिकार।
कानूनी दायरा:
IPR का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके मानसिक श्रम का पुरस्कार देना है। यह अधिकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कानूनी ढाँचों द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं।
प्रश्न 2: संक्षेप में निम्नलिखित पर नोट लिखिए।
(i) पेरिस समझौता (Paris Convention):
यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1883 में पेरिस में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक संपत्ति (जैसे- पेटेंट, ट्रेडमार्क) पर अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह समझौता सदस्यों के बीच समान नियमों को स्थापित करता है, ताकि व्यापारिक न्यायसंगतता और व्यापार बढ़ सके।
(ii) बर्न समझौता (Berne Convention):
यह 1886 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य साहित्यिक और कला कृतियों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करना था। यह समझौता यह सुनिश्चित करता है कि एक सदस्य राज्य में कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त कृति, अन्य सदस्य देशों में भी उसी सुरक्षा का हकदार होगी।
(iii) WIPO (World Intellectual Property Organization):
WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देती है। WIPO का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण करना और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
(iv) TRIPS समझौता (TRIPS Agreement):
TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करना और सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मानक निर्धारित करना है।
प्रश्न 3: कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दें।
(i) कला कृति (Artistic Work):
कला कृति में चित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि शामिल होते हैं।
(ii) नाट्य कृति (Dramatic Work):
यह किसी नाटक, अभिनय, या नृत्य कृति को कहा जाता है जिसमें संवाद, स्क्रिप्ट या प्रदर्शन शामिल हो।
(iii) सरकारी कृति (Government Work):
सरकार या इसके किसी विभाग द्वारा बनाई गई कृति।
(iv) भारतीय कृति (Indian Work):
यह कृति भारत में उत्पन्न हुई हो, चाहे इसे भारत में या बाहर प्रकाशित किया गया हो।
(v) साहित्यिक कृति (Literary Work):
यह कृतियाँ पुस्तकें, लेख, कविता, निबंध आदि होती हैं।
(vi) संगीत कृति (Musical Work):
संगीत के स्वर, संगीत के रूप में रचनाएँ, धुनें और गीत शामिल होते हैं।
(vii) लेखक (Author):
वह व्यक्ति जो किसी कृति को रचता है, चाहे वह साहित्यिक हो, संगीत हो या नाट्य कृति हो।
(viii) संगीतकार (Composer):
वह व्यक्ति जो संगीत रचनाएँ तैयार करता है।
(ix) अभिनयकर्ता (Performer):
वह व्यक्ति जो किसी कृति का प्रदर्शन करता है जैसे अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि।
(x) ध्वनि रिकॉर्डिंग (Sound Recording):
ध्वनि या संगीत को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया और उसका परिणाम।
(xi) मूर्ति (Sculpture):
कला की वह कृति जिसमें किसी सामग्री को आकार देकर किसी रूप में तराशा जाता है।
(xii) वास्तुकला कृति (Work of Architecture):
किसी भवन, संरचना या अन्य वास्तु की डिज़ाइन।
(xiii) चलचित्र (Cinematograph Film):
किसी फिल्म, वीडियो या चलचित्र का निर्माण।
(xiv) अनुकूलन (Adaptation):
किसी कृति का रूपांतरण, जैसे- नाटक से फिल्म बनाना।
(xv) उल्लंघन करने वाली प्रति (Infringing Copy):
कॉपीराइट के उल्लंघन में बनाई गई प्रति।
(xvi) संयुक्त लेखन की कृति (Work of Joint Authorship):
वह कृति जो दो या दो से अधिक लेखकों द्वारा मिलकर बनाई जाती है।
प्रश्न 4: कॉपीराइट का क्या मतलब है? क्या इसे सौंपा जा सकता है?
उत्तर:
कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी लेखक, संगीतकार, कलाकार आदि को अपनी रचनाओं पर मिलता है। यह अधिकार रचनाकार को अपनी कृति का पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन और निर्माण का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
क्या इसे सौंपा जा सकता है?
हाँ, कॉपीराइट को लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सौंपा जा सकता है। यह सौंपना (Assignment) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपनी रचना के अधिकार को पूरी तरह से या आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति को सौंपता है। यह सौंपा गया अधिकार समयसीमा और शर्तों के अनुसार हो सकता है।
प्रश्न 5: कॉपीराइट सोसाइटी क्या है? कॉपीराइट सोसाइटी के कार्यों की परीक्षा करें।
उत्तर:
कॉपीराइट सोसाइटी एक संगठन है जो कॉपीराइट धारकों के अधिकारों की रक्षा और प्रबंधन करती है। यह लेखक, संगीतकार, फिल्म निर्माता आदि के अधिकारों को एकत्र करके उनके लिए लाइसेंस जारी करती है और इसके बदले रॉयल्टी (Royalty) प्रदान करती है।
कॉपीराइट सोसाइटी के कार्य:
- कॉपीराइट धारकों के अधिकारों का प्रबंधन करना।
- रॉयल्टी संग्रह करना और उसे कॉपीराइट धारकों में वितरित करना।
- कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना।
- कॉपीराइट से संबंधित जानकारी और सलाह देना।
- कॉपीराइट के बारे में जागरूकता फैलाना।
प्रश्न 6: कॉपीराइट का पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है? क्या कॉपीराइट का पंजीकरण आवश्यक है?
उत्तर:
कॉपीराइट पंजीकरण की प्रक्रिया:
- आवेदन पत्र: पंजीकरण के लिए लेखक या उसके प्रतिनिधि को एक आवेदन पत्र भरना होता है, जो भारतीय कॉपीराइट कार्यालय (Copyright Office) में प्रस्तुत किया जाता है।
- कृति का विवरण: आवेदन पत्र में कृति का विवरण, लेखक का नाम, कृति की प्रकृति और तारीख आदि का उल्लेख करना होता है।
- प्रमाणपत्र: लेखक को कृति के असल मालिक के रूप में प्रमाणित करने के लिए उसके द्वारा कृति पर अधिकार रखने का प्रमाण देना होता है।
- साक्षात्कार: कृति की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार हो सकता है।
- पंजीकरण शुल्क: पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाता है।
क्या पंजीकरण आवश्यक है?
नहीं, कॉपीराइट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कानून के तहत, एक कृति स्वचालित रूप से कॉपीराइट से सुरक्षित होती है जब वह रचनात्मक रूप से बनाई जाती है, परंतु पंजीकरण कृति के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कानूनी पक्ष को मजबूती प्रदान करता है। पंजीकरण से कानूनी प्रक्रिया में सहूलियत होती है और पंजीकृत कॉपीराइट को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रश्न 7: कॉपीराइट का उल्लंघन क्या होता है? कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ नागरिक और आपराधिक उपायों पर चर्चा करें।
उत्तर:
कॉपीराइट उल्लंघन:
कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना लेखक या स्वामी की अनुमति के उसकी कृति का पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन या अन्यथा उपयोग करता है। यह कॉपीराइट के अधिकारों का उल्लंघन है।
नागरिक उपाय:
- न्यायालय में दावा: कॉपीराइट स्वामी अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक अदालत में दावा कर सकते हैं।
- क्षतिपूर्ति: अदालत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति (damages) की मांग कर सकती है।
आप刑िक उपाय:
- आप刑िक मामला दर्ज करना: उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
- दंड: कॉपीराइट उल्लंघन के लिए जेल की सजा (1 साल से 3 साल तक) और जुर्माना भी हो सकता है।
प्रश्न 8: निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।
(i) “कॉपीराइट एक अमूर्त अधिकार है जो लेखक को उसी की प्रतियों को बढ़ाने, प्रकाशित करने और बेचने का अधिकार देता है।” क्या यह कथन सही है?
उत्तर:
हाँ, यह कथन सही है। कॉपीराइट एक अमूर्त अधिकार है, जो लेखक को उसकी कृति की प्रतियाँ बनाने, प्रकाशित करने और बेचने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
(ii) क्या कॉपीराइट मालिक को आपराधिक उपाय उपलब्ध हैं?
उत्तर:
हाँ, कॉपीराइट मालिक के पास उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आपराधिक उपाय उपलब्ध हैं, जैसे कि जेल की सजा और जुर्माना।
(iii) क्या लेखक अपने कॉपीराइट को त्याग सकता है?
उत्तर:
हाँ, लेखक अपने कॉपीराइट को त्याग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अधिकार सभी को स्वत: ही मिल जाएगा। लेखक इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सौंप सकता है।
(iv) फोटोग्राफ के मामले में कॉपीराइट की अवधि क्या होगी?
उत्तर:
फोटोग्राफ पर कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के 60 वर्षों तक होती है।
(v) क्या कॉपीराइट के मालिक को उसमें लाइसेंस देने का अधिकार है?
उत्तर:
हाँ, कॉपीराइट का मालिक अन्य लोगों को लाइसेंस देने का अधिकार रखता है, जिससे वे उसकी कृति का उपयोग कर सकें।
(vi) क्या कॉपीराइट रजिस्टर में सुधार किया जा सकता है?
उत्तर:
हाँ, कॉपीराइट रजिस्टर में सुधार किया जा सकता है, यदि किसी त्रुटि का पता चलता है तो इसे ठीक किया जा सकता है।
(vii) लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा?
उत्तर:
लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट 60 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा।
(viii) कौन से न्यायालय कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञान में ले सकते हैं?
उत्तर:
कोर्ट ऑफ़ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय इस प्रकार के अपराधों को संज्ञान में ले सकते हैं।
(ix) कॉपीराइट उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए क्या परीक्षण होता है?
उत्तर:
कॉपीराइट उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए यह देखा जाता है कि क्या कृति का अवैध पुनरुत्पादन, वितरण, या उपयोग किया गया है, और क्या यह मौलिकता के बिना किया गया है।
प्रश्न 9: कॉपीराइट का अर्थ, विशेषताएँ और विषय-वस्तु बताएं और कॉपीराइट एक्ट, 1957 की महत्वपूर्ण विशेषताएँ बताएं।
उत्तर:
कॉपीराइट का अर्थ:
कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो लेखक या कृति के निर्माता को उनकी कृति पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार कृति के पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन, और अन्य उपयोग पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
विशेषताएँ:
- कृति का मौलिक होना: कॉपीराइट का अधिकार केवल मौलिक कृतियों पर मिलता है।
- स्वचालित सुरक्षा: जैसे ही कृति बनाई जाती है, वह स्वचालित रूप से कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित हो जाती है।
- समान अधिकार: कॉपीराइट से जुड़े अधिकार लेखक को समान रूप से सुरक्षित होते हैं, जैसे- पुनरुत्पादन, सार्वजनिक प्रदर्शन आदि।
कॉपीराइट एक्ट, 1957 की प्रमुख विशेषताएँ:
- कॉपीराइट अधिकारों की सुरक्षा।
- कॉपीराइट उल्लंघन के लिए सजा।
- कॉपीराइट सोसाइटियों का गठन।
- पंजीकरण की प्रक्रिया और दस्तावेज़।
- प्रसारण अधिकार, डाटा और सॉफ्टवेयर के अधिकार की सुरक्षा।
प्रश्न 10: क्या कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस कॉपीराइट योग्य हैं? उदाहरण के साथ यह बताएं कि क्या कॉपीराइट सुरक्षा उपलब्ध है?
उत्तर:
हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस कॉपीराइट के तहत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को एक साहित्यिक कृति माना जाता है, और यह कोड की मौलिकता के आधार पर कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित हो सकता है। डेटाबेस के लिए भी कॉपीराइट सुरक्षा मिलती है, यदि डेटाबेस की संरचना या संग्रहण में नवाचार हो।
प्रश्न 11: निम्नलिखित पर संक्षेप में नोट लिखिए।
(i) संकलन (Abridgement):
किसी कृति का संक्षिप्त रूप, जैसे कि पुस्तक का सारांश या किसी नाटक का संक्षिप्त रूप।
(ii) कॉपीराइट का हस्तांतरण (Assignment of Copyright):
कॉपीराइट मालिक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर सकता है।
(iii) न्यायोचित उपयोग (Fair Dealing):
यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत सीमित तरीके से कृतियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे- आलोचना, समीक्षा, शिक्षा आदि के लिए।
(iv) अप्रकाशित कृति (Unpublished Work):
यह वह कृति होती है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन यह फिर भी कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होती है।
(v) सार्वजनिक व्याख्यान (Public Lecture):
यह वह व्याख्यान या भाषण है जो सार्वजनिक रूप से दिया जाता है और जिस पर कॉपीराइट हो सकता है।
(vi) संग्रह (Compilation):
यह कई कृतियों या सामग्री का संग्रह है जिसे नया रूप देने के लिए व्यवस्थित किया गया है, जैसे- एन्काइकलोपीडिया।
(vii) फोटोग्राफ (Photograph):
यह एक चित्रात्मक कृति होती है जो एक कैमरे द्वारा ली जाती है और इसे कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है।
प्रश्न 11:
(viii) कॉपीराइट सुरक्षा का दायरा (Scope of Copyright Protection):
कॉपीराइट सुरक्षा केवल मौलिक कृतियों तक ही सीमित होती है, जो साहित्यिक, कला, संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्में, और कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी कृतियों में होती हैं। यह सुरक्षा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान की जाती है:
- कृति का पुनरुत्पादन: लेखक को उसकी कृति की प्रतियां बनाने का अधिकार।
- वितरण अधिकार: लेखक को अपनी कृति की कॉपियों का वितरण करने का अधिकार।
- प्रदर्शन अधिकार: कृति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने का अधिकार।
- अनुकूलन और रूपांतरण का अधिकार: कृति को अनुकूलित या रूपांतरित करने का अधिकार।
(ix) विचार कॉपीराइट से सुरक्षा प्राप्त नहीं करते (Ideas not copyrightable):
कॉपीराइट केवल मौलिक अभिव्यक्तियों की सुरक्षा करता है, विचारों या अवधारणाओं की नहीं। इसका मतलब है कि:
- विचार, सिद्धांत, तरीका, या गणना के तरीके कॉपीराइट से संरक्षित नहीं होते हैं।
- केवल विचारों की विशेष अभिव्यक्ति (जैसे लेख, चित्र आदि) को सुरक्षा मिलती है।
प्रश्न 12: “लेखक के विशेष अधिकार/सामाजिक अधिकार” (Author’s Special Rights/Moral Rights) का क्या अर्थ है? इसे समझाएं।
उत्तर:
लेखक के विशेष अधिकार (Moral Rights) उन अधिकारों को कहते हैं, जो लेखक को उसकी कृति के प्रति उसकी व्यक्तिगत जुड़ाव के आधार पर मिलते हैं। ये अधिकार निम्नलिखित होते हैं:
- पहचान का अधिकार (Right of Attribution): लेखक को अपनी कृति में अपना नाम पहचानने का अधिकार है।
- अप्रिय परिवर्तनों से बचाव (Right to Integrity): लेखक को यह अधिकार है कि उसकी कृति को बिना अनुमति के बदला या विकृत नहीं किया जा सकता।
- संशोधन का अधिकार (Right of Modification): लेखक को अपनी कृति में संशोधन करने का अधिकार है, ताकि कृति उसकी मूल भावना के अनुरूप हो।
प्रश्न 13: ‘आविष्कार’ (Invention) का क्या अर्थ है? ‘आविष्कार’ के अंतर्गत क्या नहीं आता है? और आविष्कार के शर्तें क्या हैं? स्पष्ट करें।
उत्तर:
आविष्कार (Invention) वह प्रक्रिया या वस्तु है जो तकनीकी रूप से नई, मौलिक, और औद्योगिक रूप से उपयोगी हो। इसके अंतर्गत:
- नई प्रक्रिया, उत्पाद या उपकरण जो पहले से ज्ञात न हो।
- औद्योगिक उपयोगिता होनी चाहिए।
जो आविष्कार नहीं माने जाते:
- सामान्य विचार और सिद्धांत जैसे गणना के तरीके, वैज्ञानिक सिद्धांत।
- प्राकृतिक घटनाएँ और उनके बारे में कोई नई खोज।
- कलात्मक कृतियाँ (जैसे- साहित्य, कला आदि)।
- मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक प्रक्रियाएँ।
आविष्कार की शर्तें:
- नवाचार (Novelty): आविष्कार को नया होना चाहिए, यानी इससे पहले कहीं प्रकाशित या उपयोग में न हो।
- औद्योगिक उपयोगिता (Industrial Applicability): इसका औद्योगिक उत्पादन या उपयोग संभव होना चाहिए।
- मौलिकता (Inventive Step): यह किसी सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से स्पष्ट रूप से न आने वाला होना चाहिए।
प्रश्न 14: गुप्त पेटेंट और इसके अनुदान की प्रक्रिया पर भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत चर्चा करें।
उत्तर:
गुप्त पेटेंट (Secret Patents) उन पेटेंटों को कहते हैं जिनका सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाता है। ये पेटेंट सुरक्षा कारणों से गुप्त रखे जाते हैं, जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कृतियाँ। गुप्त पेटेंट प्राप्त करने के लिए:
- पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि आविष्कार राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।
- पेटेंट कार्यालय गुप्त पेटेंट का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने से मना कर सकता है।
- पेटेंट की सुरक्षा अवधि आम तौर पर 10 वर्ष होती है, लेकिन इसमें विस्तार हो सकता है।
प्रश्न 15: पेटेंट प्राप्त करने के महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कदमों पर चर्चा करें।
उत्तर:
- आवेदन का दाखिल करना: पेटेंट आवेदन पेटेंट कार्यालय में दाखिल करना होता है।
- आविष्कार की जांच (Examination): पेटेंट कार्यालय आविष्कार की जांच करता है और यह निर्धारित करता है कि यह नया और उपयोगी है या नहीं।
- प्रकाशन: पेटेंट आवेदन को आमतौर पर 18 महीने बाद प्रकाशित किया जाता है।
- सहमति: पेटेंट आवेदन को मंजूरी दी जाती है यदि सभी शर्तों पर खरा उतरता है।
- पेटेंट का अनुदान: यदि सभी जांच पारित हो जाती हैं, तो पेटेंट प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 16: पेटेंट धारक के अधिकार और कर्तव्यों पर चर्चा करें।
उत्तर:
पेटेंट धारक के अधिकार:
- पेटेंट के अधिकार का उपयोग करना: पेटेंट धारक को अपने पेटेंट का उपयोग करने का विशेष अधिकार होता है।
- लाइसेंस देना: पेटेंट धारक अन्य व्यक्तियों को पेटेंट का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे सकता है।
- उल्लंघन पर कार्रवाई: यदि कोई अन्य व्यक्ति पेटेंट का उल्लंघन करता है, तो पेटेंट धारक इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
पेटेंट धारक के कर्तव्य:
- पेटेंट शुल्क का भुगतान: पेटेंट धारक को अपने पेटेंट के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है।
- नवीनता बनाए रखना: पेटेंट धारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका आविष्कार लगातार नया और प्रासंगिक रहे।
प्रश्न 17: पेटेंट का उल्लंघन क्या है? पेटेंट धारक के लिए उल्लंघन पर उपलब्ध उपायों पर चर्चा करें।
उत्तर:
पेटेंट उल्लंघन:
पेटेंट उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट आविष्कार का उपयोग करता है। उल्लंघन के उपाय निम्नलिखित होते हैं:
- नागरिक उपाय: पेटेंट धारक अदालत में जाकर उल्लंघनकर्ता से क्षतिपूर्ति और रुकवाने का दावा कर सकता है।
- आप刑िक उपाय: पेटेंट उल्लंघन एक आपराधिक अपराध भी हो सकता है, जिसके लिए उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना या सजा हो सकती है।
प्रश्न 18: निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:
- पेटेंट का अवधि और नवीनीकरण (Term of Patent and Renewal):
पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है। पेटेंट धारक को इस अवधि के दौरान इसे नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है, ताकि पेटेंट की सुरक्षा बनी रहे। - पेटेंट का रद्दीकरण (Revocation of Patent):
यदि पेटेंट प्राप्त करने के समय किसी धोखाधड़ी का पता चलता है या पेटेंट लागू नहीं है, तो इसे रद्द किया जा सकता है। - पेटेंट सहकारी संधि (Patent Co-operation Treaty):
यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। - पेटेंट कार्यालय (Patent Office):
यह वह सरकारी संस्था है जो पेटेंट आवेदन की समीक्षा, पंजीकरण और पेटेंट के अधिकारों की देखरेख करती है। - नियंत्रक (Controller):
यह व्यक्ति पेटेंट कार्यालय का प्रमुख होता है और पेटेंट संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है। - पेटेंट अनुदान प्रणाली का उद्देश्य (Object of Patent Grant System):
पेटेंट अनुदान प्रणाली का उद्देश्य तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और अनुसंधान तथा विकास में योगदान करना है। पेटेंट एक आविष्कारक को उसका अविष्कार प्रयोग करने और उसका व्यावसायिक लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है।
प्रश्न 19: पेटेंट एजेंट कौन है? पेटेंट एजेंट के योग्यताएँ, पंजीकरण और अधिकारों पर चर्चा करें।
उत्तर:
पेटेंट एजेंट वह व्यक्ति होता है जो पेटेंट से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ होता है और वह आवेदकों को पेटेंट आवेदन, पंजीकरण, और अन्य कानूनी कार्यों में मदद करता है।
योग्यता:
- विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।
- पेटेंट एजेंट परीक्षा में उत्तीर्ण होना।
पंजीकरण:
पेटेंट एजेंट को भारतीय पेटेंट कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है।
अधिकार:
पेटेंट एजेंट को पेटेंट आवेदन दाखिल करने, अभिप्रमाणन करने और पेटेंट के उल्लंघन के मामलों में सलाह देने का अधिकार होता है।
प्रश्न 20: पेटेंट विनिर्देशन (Patent Specification) का क्या अर्थ है? विनिर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट करें।
उत्तर:
पेटेंट विनिर्देशन पेटेंट आवेदन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें आविष्कार की विस्तृत जानकारी, उसके तकनीकी पहलू, कार्यप्रणाली और आवेदन की स्थिति होती है।
प्रकृति:
विनिर्देशन में तीन मुख्य भाग होते हैं:
- शीर्षक: आविष्कार का नाम।
- वर्णन: आविष्कार की संपूर्ण व्याख्या और इसका कार्य करने का तरीका।
- दावे (Claims): आविष्कार के विशेष हिस्सों की पहचान जो पेटेंट के तहत संरक्षित होंगे।
प्रश्न 21: ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क का पंजीकरण करने के प्रभावों पर चर्चा करें।
उत्तर:
ट्रेडमार्क एक प्रतीक, शब्द, ध्वनि, डिजाइन या अन्य पहचान चिन्ह है जो किसी उत्पाद या सेवा को अन्य समान उत्पादों या सेवाओं से अलग करता है।
पंजीकरण का प्रभाव:
- पंजीकरण से कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिससे अन्य लोग समान प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते।
- प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो व्यापार के साथ संबंध को स्पष्ट करता है।
- यदि कोई अन्य व्यक्ति ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है, तो पंजीकृत मालिक के पास उल्लंघन करने के खिलाफ कानूनी उपाय होते हैं।
प्रश्न 22: ट्रेडमार्क पंजीकरण के अस्वीकार के आधार पर चर्चा करें।
उत्तर:
ट्रेडमार्क आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है यदि:
- ट्रेडमार्क पहले से किसी अन्य का पंजीकृत है।
- ट्रेडमार्क वर्णनात्मक या गुमनाम हो।
- यह धोखाधड़ीपूर्ण है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।
- आवेदन में कोई त्रुटि हो।
प्रश्न 23: ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें।
उत्तर:
- आवेदन दाखिल करना: व्यापारी या सेवा प्रदाता ट्रेडमार्क आवेदन पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में दाखिल करता है।
- साक्षात्कार: आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर कार्यालय से संवाद किया जाता है।
- पंजीकरण: यदि ट्रेडमार्क को कोई आपत्ति नहीं होती, तो उसे पंजीकरण मिल जाता है।
प्रश्न 24: पंजीकृत ट्रेडमार्क के मालिक के अधिकारों पर चर्चा करें।
उत्तर:
- अन्य के उपयोग को रोकना: ट्रेडमार्क मालिक को अपने ट्रेडमार्क का बिना अनुमति के उपयोग को रोकने का अधिकार है।
- विकास और विस्तार: ट्रेडमार्क मालिक अपने व्यापार या उत्पाद का विस्तार करने में सक्षम होता है।
सीमाएँ: - अवधि: ट्रेडमार्क की सुरक्षा अवधि 10 साल होती है, जो बाद में नवीनीकरण के साथ बढ़ाई जा सकती है।
- भूगोल: पंजीकरण विशेष क्षेत्र या देश के लिए होता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए अन्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
प्रश्न 25: ट्रेडमार्क का हस्तांतरण और प्रसारण पर चर्चा करें। क्या हस्तांतरण या प्रसारण का पंजीकरण अनिवार्य है?
उत्तर:
- हस्तांतरण (Assignment): ट्रेडमार्क मालिक अपने अधिकारों को अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है।
- प्रसारण (Transmission): जब ट्रेडमार्क का स्वामित्व बदलता है, तो उसे प्रसारित किया जा सकता है, जैसे कि उत्तराधिकार में।
पंजीकरण:
हां, हस्तांतरण या प्रसारण का पंजीकरण अनिवार्य है, ताकि अधिकारों का वैधता साबित हो सके।
प्रश्न 26: पंजीकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। या लाइसेंसिंग समझौता क्या है? लाइसेंसिंग समझौते को कैसे पंजीकृत किया जा सकता है?
उत्तर:
पंजीकृत उपयोगकर्ता (Registered User) का पंजीकरण:
ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत, पंजीकृत उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे ट्रेडमार्क के मालिक द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग का अधिकार दिया गया हो। पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:
- आवेदन दाखिल करना: ट्रेडमार्क का मालिक या इच्छुक उपयोगकर्ता ट्रेडमार्क पंजीकरण कार्यालय में आवेदन दाखिल करता है।
- पंजीकरण की स्वीकृति: आवेदन के निरीक्षण के बाद, यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो पंजीकृत उपयोगकर्ता का पंजीकरण किया जाता है।
- दावों का निवारण: यदि आवेदन में कोई आपत्ति होती है, तो उसे निवारण किया जाता है और पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
लाइसेंसिंग समझौता (Licensing Agreement):
लाइसेंसिंग समझौता एक कानूनी अनुबंध है, जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, या डिजाइन। यह समझौता विभिन्न प्रकार से हो सकता है:
- विशेष लाइसेंस (Exclusive License)
- गैर-विशेष लाइसेंस (Non-exclusive License)
लाइसेंसिंग समझौते का पंजीकरण:
लाइसेंसिंग समझौते को ट्रेडमार्क, पेटेंट या डिजाइन अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया में:
- संबंधित कार्यालय में लाइसेंसिंग समझौते का आवेदन दाखिल किया जाता है।
- पंजीकरण के बाद, लाइसेंसिंग समझौते को वैधता प्राप्त होती है और इसका कानूनी संरक्षण किया जाता है।
प्रश्न 27: ट्रेडमार्क उल्लंघन के उपायों पर चर्चा करें।
उत्तर:
ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए निम्नलिखित कानूनी उपाय उपलब्ध हैं:
- नागरिक उपाय (Civil Remedies):
- अदालत में मुकदमा: उल्लंघनकर्ता के खिलाफ नुकसान का दावा किया जा सकता है।
- स्थगन आदेश (Injunction): अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त किया जा सकता है ताकि उल्लंघनकर्ता को आगे व्यापार में वही ट्रेडमार्क उपयोग करने से रोका जा सके।
- क्षतिपूर्ति: उल्लंघनकर्ता से उत्पन्न होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है।
- आप刑िक उपाय (Criminal Remedies):
- यदि ट्रेडमार्क उल्लंघन धोखाधड़ी का हिस्सा है, तो उल्लंघनकर्ता को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
- उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है जो विशेष रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में लागू होता है।
प्रश्न 28: पासिंग ऑफ (Passing Off) का स्वरूप और दायरा क्या है? पासिंग ऑफ के मामले में धोखाधड़ी का परीक्षण कैसे किया जाता है?
उत्तर:
पासिंग ऑफ (Passing Off):
पासिंग ऑफ तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा के लिए किसी अन्य की ट्रेडमार्क, नाम, या अन्य पहचान चिन्ह का गलत तरीके से उपयोग करता है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता है। यह आमतौर पर गैर-पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के रूप में होता है।
दायरा:
- व्यापारिक पहचान का उल्लंघन: किसी अन्य की प्रतिष्ठा और व्यापारिक पहचान का नकल करना।
- उपभोक्ताओं को धोखा देना: उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाना कि एक उत्पाद या सेवा किसी अन्य से संबंधित है।
धोखाधड़ी का परीक्षण:
धोखाधड़ी का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है:
- पहचान का समानता: क्या दोनों उत्पादों के बीच कोई समानता है जो उपभोक्ता को भ्रमित कर सकती है?
- सार्वजनिक भ्रम: क्या उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है कि ये दोनों एक ही निर्माता या सेवा प्रदाता से संबंधित हैं?
- व्यापारिक पहचान की हानि: क्या ट्रेडमार्क की गलत पहचान से व्यापार को नुकसान हो सकता है?
प्रश्न 29: ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर:
ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 भारत में ट्रेडमार्क की सुरक्षा और पंजीकरण से संबंधित कानून है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- पंजीकरण प्रक्रिया: यह अधिनियम पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाता है।
- ट्रेडमार्क के अधिकार: यह पंजीकृत ट्रेडमार्क मालिक को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- सुरक्षा: ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और उपायों का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा: यह अधिनियम न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडमार्क के अधिकारों की रक्षा करता है।
- क्षेत्रीय पंजीकरण: यह अधिनियम क्षेत्रीय पंजीकरण की भी अनुमति देता है, जिससे एक ट्रेडमार्क का उपयोग विभिन्न राज्यों में किया जा सकता है।
प्रश्न 30: निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:
(i) ट्रेडमार्क सुरक्षा- कारण (Trade Mark Protection – Reasons for):
ट्रेडमार्क सुरक्षा का उद्देश्य व्यापारिक पहचान की रक्षा करना है, ताकि उपभोक्ताओं को सही उत्पाद या सेवा का चयन करने में मदद मिल सके और व्यापारिक प्रतिष्ठा का संरक्षण हो सके।
(ii) सामूहिक चिह्न (Collective Marks):
यह एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो एक समूह के सदस्य द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे सहकारी संस्थाएँ या संघ। इसका उद्देश्य समूह के उत्पादों या सेवाओं को पहचानना है।
(iii) प्रमाणन चिह्न (Certification of Trade Marks):
यह चिह्न यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद ने विशेष गुणवत्ता या मानक को पूरा किया है, जैसे किसी उत्पाद का जैविक होना।
(iv) प्रसिद्ध ट्रेडमार्क (Well-known Trade Mark):
यह ट्रेडमार्क किसी विशेष उत्पाद या सेवा से संबंधित इतना प्रसिद्ध होता है कि उपभोक्ता इसे तुरंत पहचान लेते हैं, भले ही उसका उपयोग कहीं और क्यों न हो।
(v) डोमेन नाम (Domain Name):
डोमेन नाम इंटरनेट पर एक वेबसाइट की पहचान होता है और यह ट्रेडमार्क के समान सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न 31: ‘डिजाइन’ का क्या अर्थ है? डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? कौन से डिज़ाइन पंजीकरण के लिए योग्य नहीं होते?
उत्तर:
डिजाइन:
डिजाइन किसी उत्पाद की बाहरी आकृति, पैटर्न, आकार, रंग या सजावट को दर्शाता है। यह एक विशेषता होती है जो किसी उत्पाद को अद्वितीय बनाती है।
डिज़ाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
- आवेदन दाखिल करना: डिज़ाइन पंजीकरण के लिए आवेदन पेटेंट कार्यालय में किया जाता है।
- आवेदन की जांच: पेटेंट कार्यालय डिज़ाइन का निरीक्षण करता है, और यदि डिज़ाइन नए और मौलिक होते हैं तो इसे पंजीकृत किया जाता है।
- पंजीकरण की स्वीकृति: यदि डिज़ाइन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
जो डिज़ाइन पंजीकरण योग्य नहीं हैं:
- प्राकृतिक रूप: प्राकृतिक तत्वों जैसे- रूप, आकार जो पहले से अस्तित्व में हैं।
- रंग संयोजन: केवल रंग संयोजन के कारण कोई डिज़ाइन पंजीकृत नहीं हो सकता।
- असामान्य रूप: ऐसा डिज़ाइन जो किसी निश्चित नियम या रूप का पालन नहीं करता हो।
प्रश्न 32: निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें:
- आर्टिकल (Article): वह वस्तु जो एक डिजाइन के लिए आवेदन करती है, जैसे कपड़े, गहने, आदि।
- नियंत्रक (Controller): पेटेंट कार्यालय में वह अधिकारी जो पंजीकरण प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- कॉपीराइट (Copyright): एक कानूनी अधिकार जो रचनात्मक कृतियों की मूल अभिव्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है।
- कानूनी प्रतिनिधि (Legal Representative): वह व्यक्ति जो किसी मृतक की संपत्ति का प्रबंधन करता है।
- मौलिक (Original): कोई कृति या डिज़ाइन जो नवीन और बिना नकल के हो।
- नई या मौलिक डिज़ाइन का मालिक (Proprietor of new or original design): वह व्यक्ति जो नई और मौलिक डिज़ाइन का स्वामी होता है।
प्रश्न 33: पंजीकृत डिज़ाइनों में कॉपीराइट कानून से संबंधित क्या है?
उत्तर:
पंजीकृत डिज़ाइन का एक कॉपीराइट भी हो सकता है, विशेष रूप से अगर डिज़ाइन की कोई रचनात्मक और कला संबंधी अभिव्यक्ति हो। पंजीकरण से डिज़ाइन को कॉपीराइट से सुरक्षा प्राप्त होती है।
प्रश्न 34: पंजीकृत डिज़ाइन के मालिक को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं?
उत्तर:
पंजीकृत डिज़ाइन के मालिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:
- एक्सक्लूसिव अधिकार (Exclusive Rights):
पंजीकरण के बाद, डिज़ाइन का मालिक केवल उसे उपयोग करने का अधिकार रखता है। कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के उस डिज़ाइन का उपयोग नहीं कर सकता। - नकल करने से रोक (Prevention of Copying):
मालिक को यह अधिकार होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी डिज़ाइन की नकल करने से रोक सकता है। - सुरक्षा का अधिकार (Protection Rights):
पंजीकृत डिज़ाइन को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे मालिक उसे अन्य व्यक्तियों से बचा सकता है जो बिना अनुमति के डिज़ाइन का उपयोग करते हैं। - लाइसेंसिंग और ट्रांसफर (Licensing and Transfer Rights):
डिज़ाइन का मालिक अपने डिज़ाइन के अधिकार को लाइसेंस के रूप में अन्य व्यक्तियों को दे सकता है, या इसे दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है। - विक्री अधिकार (Commercial Rights):
पंजीकृत डिज़ाइन को अन्य उत्पादों या सेवाओं के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के अधिकार होते हैं।
प्रश्न 35: डिज़ाइन में कॉपीराइट का उल्लंघन क्या है? डिज़ाइन में कॉपीराइट की चोरी के खिलाफ कौन से उपाय उपलब्ध हैं?
उत्तर:
कॉपीराइट की चोरी (Piracy of Copyright in Design):
डिज़ाइन में कॉपीराइट की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पंजीकृत डिज़ाइन की नकल करता है या उसकी अवैध प्रतियां बनाता है, जो कि डिज़ाइन के मालिक के अधिकारों का उल्लंघन है। यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है और कानूनी रूप से दंडनीय होती है।
कॉपीराइट की चोरी के खिलाफ उपाय:
- नागरिक उपाय (Civil Remedies):
- स्थगन आदेश (Injunction): डिज़ाइन मालिक अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है, जिससे उल्लंघनकर्ता को डिज़ाइन का उपयोग करने से रोका जा सके।
- नुकसान की भरपाई (Damages): डिज़ाइन मालिक उल्लंघनकर्ता से उस नुकसान की भरपाई का दावा कर सकता है, जो उसे चोरी से हुआ हो।
- आप刑िक उपाय (Criminal Remedies):
- जुर्माना और सजा: डिज़ाइन चोरी पर उल्लंघनकर्ता को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
- जांच और अभियोजन: पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारी उल्लंघन की जांच कर सकते हैं और आरोपी के खिलाफ अभियोजन शुरू कर सकते हैं।
प्रश्न 36: ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें डिज़ाइन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है?
उत्तर:
डिज़ाइन का पंजीकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:
- डिज़ाइन की नवीनता और मौलिकता का अभाव (Lack of Novelty and Originality):
यदि यह साबित हो कि डिज़ाइन नया और मौलिक नहीं है, यानी यह पहले से कहीं और उपयोग में था या पहले से प्रकाशित था, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। - वर्तमान पंजीकरण का गलत रूप से किया गया आवेदन (False Representation of Registration):
यदि डिज़ाइन मालिक ने गलत जानकारी दी हो, या पंजीकरण के दौरान धोखाधड़ी की हो, तो डिज़ाइन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। - नियमों का उल्लंघन (Violation of Registration Rules):
यदि डिज़ाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, तो डिज़ाइन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। - डिज़ाइन का सार्वजनिक उपयोग (Public Use of Design):
यदि डिज़ाइन का पंजीकरण के बाद सार्वजनिक रूप से उपयोग शुरू हो गया हो और डिज़ाइन का मालिक इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। - न्यायिक आदेश (Judicial Order):
किसी अदालत या सक्षम प्राधिकरण द्वारा यह आदेश दिए जाने पर डिज़ाइन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। - पंजीकरण के बाद अनधिकृत परिवर्तन (Unauthorized Changes After Registration):
यदि पंजीकरण के बाद डिज़ाइन में कोई अनधिकृत परिवर्तन किया गया हो, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
प्रश्न 37: डिज़ाइन्स एक्ट, 2000 के तहत नियंत्रक के अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा करें।
उत्तर:
डिज़ाइन्स एक्ट, 2000 के तहत नियंत्रक (Controller) के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जिनमें:
- पंजीकरण का प्राधिकरण (Authority for Registration):
नियंत्रक को डिज़ाइन के पंजीकरण के आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि डिज़ाइन सभी कानूनी मानकों और शर्तों के अनुसार पंजीकृत हो। - पंजीकरण के बाद के कार्य (Post-Registration Duties):
वह डिज़ाइनों के पंजीकरण के बाद, उनकी वैधता की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डिज़ाइन के अधिकारों का उल्लंघन न हो। - मंजूरी और नवीकरण (Approval and Renewal):
डिज़ाइन के पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर, नियंत्रक के पास डिज़ाइन का नवीकरण करने का अधिकार होता है। - विरोध और दावों का समाधान (Opposition and Dispute Resolution):
नियंत्रक पंजीकरण के विरोधों और संबंधित दावों का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि डिज़ाइन से संबंधित सभी विवादों का उचित तरीके से समाधान हो। - नियमों और दिशानिर्देशों का पालन (Adherence to Rules and Guidelines):
नियंत्रक डिज़ाइन पंजीकरण के लिए निर्धारित सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है। - दंड और जुर्माना (Penalty and Fine):
यदि कोई व्यक्ति डिज़ाइन पंजीकरण के कानून का उल्लंघन करता है, तो नियंत्रक उस पर दंड और जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है।
प्रश्न 38: डिज़ाइन्स एक्ट, 2000 की मुख्य विशेषताएँ वर्णन करें।
उत्तर:
डिज़ाइन्स एक्ट, 2000 भारत में डिज़ाइन की पंजीकरण, संरक्षण और उल्लंघन से संबंधित कानूनी प्रावधानों को निर्धारित करता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- डिज़ाइन का पंजीकरण (Registration of Designs):
डिज़ाइन एक्ट, 2000 के तहत, एक डिज़ाइन का पंजीकरण केवल तब किया जा सकता है जब वह नया, मौलिक और दृश्यात्मक रूप में आकर्षक हो। - पंजीकरण की अवधि (Duration of Registration):
डिज़ाइन का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, और इसे एक बार नवीनीकरण के द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। - डिज़ाइन की चोरी और उल्लंघन (Infringement and Piracy of Designs):
डिज़ाइन के पंजीकरण से, मालिक को अपनी डिज़ाइन की नकल और उल्लंघन से सुरक्षा मिलती है, और उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। - विरोध का प्रावधान (Provision for Opposition):
डिज़ाइन पंजीकरण के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा विरोध दर्ज कराया जा सकता है, और नियंत्रक इसके समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकता है। - अंतर्राष्ट्रीय मान्यता (International Recognition):
डिज़ाइन एक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन के अधिकारों की रक्षा करता है और इसमें पेरिस समझौते के अंतर्गत डिज़ाइन के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा दी जाती है। - आवेदन की प्रक्रिया (Application Process):
डिज़ाइन पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिसमें आवेदन को डिज़ाइन के अद्वितीय रूप, प्रकार और उपयोग की जानकारी देना होता है।
प्रश्न 39: भौगोलिक संकेतों (Geographical Indications) की वस्तुओं (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की मुख्य विशेषताएँ वर्णन करें।
उत्तर:
भौगोलिक संकेतों (Geographical Indications) की वस्तुओं (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का उद्देश्य भारत में उत्पादों के भौगोलिक संकेतों के संरक्षण और पंजीकरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:
- भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण (Registration of Geographical Indications):
भौगोलिक संकेतों को पंजीकृत किया जाता है जो किसी विशेष स्थान, क्षेत्र या राज्य से जुड़े होते हैं और जहां का उत्पाद वहां की विशेषता या गुणवत्ता को दर्शाता है। - भौगोलिक संकेतों का संरक्षण (Protection of Geographical Indications):
इस अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे अन्य कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से उपयोग न किए जा सकें। - पंजीकरण की प्रक्रिया (Registration Process):
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था को यह साबित करना होता है कि उत्पाद विशिष्ट स्थान से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा उस स्थान से जुड़ी हुई है। - आधिकारिक आयोग (Geographical Indications Registry):
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के लिए एक आधिकारिक आयोग स्थापित किया गया है, जो पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करता है और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। - नौकरियों के लिए प्रेरणा (Incentives for Employment):
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण से संबंधित उद्योगों और क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन होता है, जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ होता है।
प्रश्न 40: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें।
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य भारत की जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और उपयोग को नियंत्रित करना है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- संविधान और उद्देश्य (Constitution and Purpose):
जैव विविधता अधिनियम का उद्देश्य जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का गैर-वैज्ञानिक या असंवेदनशील उपयोग न हो। - संविधान की प्रक्रिया (Constitutional Process):
इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों की स्थापना की गई है, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। - जैविक संसाधनों का उपयोग (Use of Biological Resources):
यह अधिनियम जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित करता है, खासकर जब यह संसाधन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। - बायोपायरेसी (Biopiracy) का विरोध (Opposition to Biopiracy):
अधिनियम जैव संसाधनों की चोरी और अनुचित तरीके से उपयोग करने के खिलाफ प्रावधान देता है, जो कि जैविक विविधता की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।
प्रश्न 41: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों की संविधान और शक्तियों का वर्णन करें, जैसा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 में निर्धारित किया गया है।
उत्तर:
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों की संविधान और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority):
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन जैव विविधता के राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण, सुरक्षा और उपयोग के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख कार्यों में जैव संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति देना, जैव विविधता का संरक्षण करना और जैविक संसाधनों की अनुचित व्यापारिक उपयोग को रोकना शामिल हैं। - राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Boards):
राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्यों में जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बोर्ड राज्य स्तर पर जैव विविधता की रक्षा, जागरूकता फैलाने और स्थानीय समुदायों को जैव विविधता के महत्व के बारे में सूचित करने का कार्य करते हैं।
यहां प्रश्न 42 से 60 तक के उत्तर विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 42: जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है?
उत्तर:
जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इन संसाधनों का अति प्रयोग न हो और उनका नुकसान न हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:
- स्थानीय समुदायों से सहमति (Prior Informed Consent):
जैविक संसाधनों का उपयोग करने से पहले स्थानीय समुदायों से अनुमति ली जानी चाहिए, जो इन संसाधनों के पारंपरिक उपयोगकर्ता होते हैं। - सतत उपयोग (Sustainable Use):
जैव संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए, जो उनका संरक्षण और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करे। इसका मतलब यह है कि इन संसाधनों का उपयोग उनकी जनसंख्या को नुकसान न पहुँचाए। - पारदर्शिता और न्याय (Transparency and Equity):
जैव संसाधनों का उपयोग करते समय पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि सभी संबंधित पक्षों को उनके अधिकारों का सम्मान मिले और उन्हें उचित लाभ प्राप्त हो।
प्रश्न 43: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य बायोपायरेसी (Biopiracy) को रोकना है?
उत्तर:
जी हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 का एक प्रमुख उद्देश्य बायोपायरेसी को रोकना है। बायोपायरेसी का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का गैरकानूनी तरीके से वाणिज्यिक उपयोग। जैव विविधता अधिनियम इस प्रकार के कृत्यों के खिलाफ कानूनी उपायों को सुनिश्चित करता है और बायोपायरेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है।
प्रश्न 44: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध है?
उत्तर:
हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत, जैव संसाधनों के निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है, खासकर यदि संसाधन वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्यात किए जा रहे हों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों का संरक्षण किया जाए और उनका अनुचित उपयोग न हो।
प्रश्न 45: जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैव विविधता के लिए कार्ययोजना क्या है?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना का उद्देश्य जैविक संसाधनों का समुचित संरक्षण करना, उनका स्थिरता से उपयोग करना और जैव विविधता से जुड़ी जानकारी को संरक्षित करना है। इसके अंतर्गत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए हैं, जैसे:
- जैव विविधता के संरक्षण के लिए योजना बनाना।
- स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना।
- जैव विविधता पर संकटग्रस्त प्रजातियों की निगरानी।
प्रश्न 46: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रमुख कार्य क्या हैं?
उत्तर:
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- जैव विविधता के संरक्षण का मार्गदर्शन करना।
- जैव संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति देना और उसका निगरानी करना।
- बायोपायरेसी के मामलों की जांच करना और कार्रवाई करना।
- जैव विविधता के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाना।
- संबंधित पक्षों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
प्रश्न 47: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए किस प्रकार की सहमति की आवश्यकता होती है?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए “पूर्व सूचित सहमति” (Prior Informed Consent) की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जैव संसाधनों का उपयोग करने से पहले संबंधित स्थानीय समुदायों और जनजातियों से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, जो इन संसाधनों के पारंपरिक उपयोगकर्ता होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संसाधनों के उपयोग से समुदाय को उचित लाभ और सम्मान मिले।
प्रश्न 48: भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के लाभ क्या हैं?
उत्तर:
भौगोलिक संकेतों (Geographical Indications) के पंजीकरण के कई लाभ हैं, जिनमें:
- वाणिज्यिक लाभ (Commercial Advantage):
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण से उत्पाद की विशिष्टता और गुणवत्ता को मान्यता मिलती है, जिससे उत्पाद की बिक्री और प्रसिद्धि बढ़ती है। - संरक्षण और सुरक्षा (Protection and Security):
पंजीकरण से भौगोलिक संकेतों को धोखाधड़ी और अनुचित उपयोग से सुरक्षा मिलती है। - स्थानीय समुदायों को लाभ (Benefit to Local Communities):
यह पंजीकरण स्थानीय उत्पादकों को उनके उत्पादों की पहचान और उनका उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।
प्रश्न 49: क्या जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक विदेशी व्यक्ति को जैव संसाधन उपयोग की अनुमति मिल सकती है?
उत्तर:
जी हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत विदेशी व्यक्ति को जैव संसाधन के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि विदेशी व्यक्ति जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें उचित अधिकार प्राप्त करना होगा और जैव विविधता से संबंधित कोई भी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना होगा।
प्रश्न 50: जैव विविधता अधिनियम, 2002 में बायोपायरेसी के खिलाफ क्या प्रावधान हैं?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 में बायोपायरेसी के खिलाफ कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- स्रोत की पहचान (Identification of Source):
यदि कोई व्यक्ति किसी जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग करना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसने वह संसाधन सही स्रोत से लिया है और उसने स्थानीय समुदायों से सहमति प्राप्त की है। - बायोपायरेसी के मामलों की जांच (Investigation of Biopiracy Cases):
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को बायोपायरेसी के मामलों की जांच करने का अधिकार है और वह इस पर कार्रवाई करता है। - पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण (Conservation of Traditional Knowledge):
बायोपायरेसी को रोकने के लिए पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है, ताकि यह ज्ञान गैरकानूनी तरीके से न लिया जाए।
यहां प्रश्न 51 से 60 के उत्तर विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 51: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत “संवेदनशील जैव विविधता” को परिभाषित करें।
उत्तर:
संवेदनशील जैव विविधता का तात्पर्य उन जैविक संसाधनों और प्रजातियों से है जो संकटग्रस्त हैं या जिन्हें संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। यह ऐसी प्रजातियाँ हो सकती हैं जो प्रदूषण, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। ऐसे संसाधनों के लिए विशिष्ट संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है ताकि उनकी विलुप्ति को रोका जा सके।
प्रश्न 52: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कार्यों को स्पष्ट करें।
उत्तर:
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के कार्य निम्नलिखित हैं:
- संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति देना:
NBA, जैव संसाधनों के उपयोग और उनके वाणिज्यिक प्रयोग के लिए स्थानीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर अनुमति देता है। - जैव विविधता का संरक्षण:
यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाता है और उसे लागू करता है। - बायोपायरेसी के खिलाफ कार्रवाई:
बायोपायरेसी (biopiracy) के मामलों की जांच करता है और यदि कोई बायोपायरेसी का मामला पाया जाता है, तो वह कानूनी कार्रवाई करता है। - जैव विविधता का प्रचार-प्रसार:
यह जैव विविधता के महत्व को समझाने और उसे बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
प्रश्न 53: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक व्यक्ति जैव संसाधन का उपयोग करने से पहले पूर्व सहमति प्राप्त कर सकता है?
उत्तर:
हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव संसाधन का उपयोग करने से पहले संबंधित स्थानीय समुदायों या पारंपरिक ज्ञान के मालिकों से “पूर्व सूचित सहमति” (Prior Informed Consent) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि जैव संसाधनों का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए और स्थानीय समुदायों को उनके संसाधनों का लाभ मिले।
प्रश्न 54: जैव विविधता अधिनियम, 2002 में ‘निर्यात’ से संबंधित क्या प्रावधान हैं?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के निर्यात पर प्रावधान हैं, जिनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जैव संसाधन का निर्यात करना चाहता है, तो उसे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जैव संसाधनों का निर्यात अवैध तरीके से न हो और इसका उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए।
प्रश्न 55: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर:
जी हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित समुदायों से पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, जैव संसाधनों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका लाभ उस समुदाय को मिलेगा और इसे स्थायी तरीके से किया जाएगा।
प्रश्न 56: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के अवैध वाणिज्यिक उपयोग पर कोई प्रावधान है?
उत्तर:
जी हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के अवैध वाणिज्यिक उपयोग पर कड़े प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जैव संसाधनों का बिना अनुमति के उपयोग करती है, तो वह बायोपायरेसी (biopiracy) के अंतर्गत आता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, प्राधिकरण जैव संसाधनों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए निगरानी रखता है।
प्रश्न 57: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 का मुख्य उद्देश्य बायोपायरेसी (Biopiracy) को रोकना है?
उत्तर:
जी हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 का मुख्य उद्देश्य बायोपायरेसी को रोकना है। बायोपायरेसी का मतलब है जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का अवैध तरीके से उपयोग करना। इस अधिनियम के तहत, जैव संसाधनों का उपयोग करने से पहले स्थानीय समुदायों से अनुमति लेना अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार की बायोपायरेसी को रोका जा सके।
प्रश्न 58: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया है?
उत्तर:
हां, जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए उसे जैव संसाधनों के उपयोग की योजना प्रस्तुत करनी होती है और यह साबित करना होता है कि उसने संबंधित समुदायों से पूर्व सहमति प्राप्त की है।
प्रश्न 59: भौगोलिक संकेतों (Geographical Indications) के पंजीकरण के लाभ क्या हैं?
उत्तर:
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के कई लाभ हैं, जिनमें:
- वाणिज्यिक लाभ:
पंजीकरण से उत्पाद की विशिष्टता और गुणवत्ता की पुष्टि होती है, जिससे उत्पाद की बिक्री बढ़ती है और यह प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान प्राप्त करता है। - संरक्षण और सुरक्षा:
यह पंजीकरण उत्पादों की सुरक्षा करता है और उनके अनाधिकृत उपयोग से बचाता है। - स्थानीय समुदायों को लाभ:
यह स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है।
प्रश्न 60: क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 में जैविक संसाधनों के निर्यात पर कोई शुल्क लागू होता है?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैविक संसाधनों के निर्यात पर शुल्क लागू हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित शुल्क और अन्य नियमों का पालन करना होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैव संसाधनों का निर्यात स्थायी तरीके से किया जाए और उनका सही उपयोग हो।
यहां प्रश्न 61 से 80 तक के उत्तर विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 61: भौगोलिक संकेत (Geographical Indication) क्या है? इसे किस प्रकार पंजीकृत किया जा सकता है?
उत्तर:
भौगोलिक संकेत (GI) वह चिन्ह है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान से संबंधित उत्पादों को चिन्हित करता है, जिनकी गुणवत्ता या अन्य विशेषताएँ उस क्षेत्र या स्थान के पर्यावरणीय या सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। इसे पंजीकरण के लिए भारतीय भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, 1999 के तहत आवेदन करना होता है। पंजीकरण के लिए उत्पाद के संबंधित क्षेत्रीय पहचान और उत्पाद की विशेषताओं को साबित करना होता है।
प्रश्न 62: भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण से क्या लाभ होते हैं?
उत्तर:
भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के निम्नलिखित लाभ होते हैं:
- संरक्षण:
यह उत्पाद की विशिष्टता को कानूनी रूप से संरक्षित करता है और उसके नाम का अवैध उपयोग रोकता है। - वाणिज्यिक लाभ:
उत्पाद की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, जिससे बाजार में उसकी पहचान मजबूत होती है। - स्थानीय समुदायों का लाभ:
उत्पादों के पंजीकरण से स्थानीय उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिलता है और उन्हें व्यावसायिक पहचान मिलती है।
प्रश्न 63: डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत डिज़ाइन का पंजीकरण कैसे किया जाता है?
उत्तर:
डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत डिज़ाइन पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- आवेदन दाखिल करना:
डिज़ाइन का पंजीकरण आवेदन भारतीय डिजाइन कार्यालय में दाखिल किया जाता है। - पंजीकरण की जांच:
आवेदन के बाद डिज़ाइन की जांच की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह नया और मौलिक है। - पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना:
यदि डिज़ाइन को सभी मानकों पर खरा पाया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न 64: डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत “डिज़ाइन” की परिभाषा क्या है?
उत्तर:
डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत, डिज़ाइन वह किसी वस्तु के बाहरी रूप, आकार, रेखा, रंग, बनावट या सामग्री का संयोजन है, जिसे दृश्य रूप से देखा जा सकता है और जो औद्योगिक रूप से पुन: उत्पादित किया जा सकता है। डिज़ाइन का उद्देश्य उत्पाद की आंतरिक कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं करना है, बल्कि केवल उसके दृश्य रूप को सुधारना है।
प्रश्न 65: डिज़ाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
उत्तर:
डिज़ाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं:
- नवीनता: डिज़ाइन नया और मौलिक होना चाहिए।
- दृश्यता: डिज़ाइन को देखने में स्पष्ट और दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हो।
- पुनरुत्पादन: डिज़ाइन को औद्योगिक दृष्टि से पुन: उत्पादित किया जा सकता हो।
प्रश्न 66: डिज़ाइन के अधिकारों का उल्लंघन (Piracy of Design) क्या है? और इससे बचने के उपाय?
उत्तर:
डिज़ाइन के अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब किसी व्यक्ति या संस्था किसी पंजीकृत डिज़ाइन को अनुमति के बिना नकल करती है या उसका उपयोग करती है। इसे पाइरेसी कहा जाता है। इसके खिलाफ उपायों में पंजीकरण करवाना, डिज़ाइन के मालिकाना अधिकार का संरक्षण करना और कानूनी कार्यवाही करना शामिल है।
प्रश्न 67: डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकरण के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं?
उत्तर:
डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:
- आवेदन दाखिल करना:
डिज़ाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन भारतीय डिज़ाइन कार्यालय में दाखिल किया जाता है। - जांच प्रक्रिया:
डिज़ाइन की नवीनता और मौलिकता की जांच की जाती है। - पंजीकरण:
डिज़ाइन के सफल परीक्षण के बाद, डिज़ाइन को पंजीकृत किया जाता है और प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न 68: डिज़ाइन पंजीकरण का क्या महत्व है?
उत्तर:
डिज़ाइन पंजीकरण का महत्व यह है कि यह उत्पाद के डिज़ाइन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। इससे डिज़ाइन का अवैध उपयोग रोका जा सकता है, और डिज़ाइन के मालिक को विशेष अधिकार मिलते हैं, जो उसकी मौलिकता और व्यवसायिकता को सुनिश्चित करते हैं।
प्रश्न 69: “पेटेंट” और “डिज़ाइन” में क्या अंतर है?
उत्तर:
पेटेंट और डिज़ाइन में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
- पेटेंट:
पेटेंट एक तकनीकी या वैज्ञानिक आविष्कार पर दिया जाता है, जो नई और उपयोगी हो। पेटेंट का उद्देश्य आविष्कारक के अधिकारों का संरक्षण करना है। - डिज़ाइन:
डिज़ाइन एक उत्पाद के दृश्य रूप, आकार, बनावट या रंग पर आधारित होता है, जो औद्योगिक रूप से पुन: उत्पादित किया जा सकता है। डिज़ाइन का उद्देश्य केवल दृश्य आकर्षण को बढ़ाना है।
प्रश्न 70: पेटेंट अधिनियम के तहत “आविष्कार” की परिभाषा क्या है?
उत्तर:
पेटेंट अधिनियम के तहत, “आविष्कार” एक नई प्रक्रिया, यंत्र, उपकरण, पदार्थ, या इसके किसी अन्य रूप का संयोजन होता है, जो उपयोगी हो और उसकी तकनीकी प्रकृति हो। यह एक ऐसी तकनीकी सोच या नवाचार है जिसे पहले नहीं किया गया हो और जो उपयोगी हो।
प्रश्न 71: पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:
- आविष्कार का दस्तावेजीकरण:
पहले आविष्कार का पूरा विवरण और उसका तकनीकी समाधान तैयार करना होता है। - आवेदन दाखिल करना:
पेटेंट आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जाता है। - परीक्षण:
आवेदन के बाद, पेटेंट कार्यालय द्वारा आविष्कार की नवीनता और उपयोगिता की जांच की जाती है। - पेटेंट जारी करना:
यदि आविष्कार सभी मानकों पर खरा उतरता है, तो पेटेंट प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
प्रश्न 72: पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन (Infringement of Patent Rights) क्या है और इसके खिलाफ उपाय?
उत्तर:
पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पेटेंट प्राप्त आविष्कार का बिना अनुमति के उपयोग किया जाता है। इसके खिलाफ उपायों में कानूनी कार्यवाही करना, पेटेंट की सुरक्षा के लिए न्यायालय में मामला दर्ज करना, और मुआवजे की मांग करना शामिल है।
प्रश्न 73: पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन से बचने के उपाय क्या हैं?
उत्तर:
पेटेंट अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
- पेटेंट पंजीकरण:
आविष्कार को पेटेंट के रूप में पंजीकृत करना। - निगरानी रखना:
पेटेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेटेंट की निगरानी रखना और अवैध उपयोग की जांच करना। - कानूनी कार्रवाई:
उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करना और मुआवजा प्राप्त करना।
प्रश्न 74: पेटेंट की समाप्ति अवधि क्या होती है?
उत्तर:
पेटेंट की समाप्ति अवधि आमतौर पर 20 वर्ष होती है, जिसके बाद पेटेंट का अधिकार समाप्त हो जाता है और आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में चला जाता है। कुछ मामलों में, पेटेंट की अवधि को एक बार नवीनीकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
प्रश्न 75: किसी पेटेंट के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
उत्तर:
पेटेंट पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें हैं:
- नवीनता:
आविष्कार नया और पहले से ज्ञात नहीं होना चाहिए। - उपयोगिता:
आविष्कार उपयोगी होना चाहिए और किसी समस्या का समाधान प्रदान करना चाहिए। - मौलिकता:
आविष्कार मौलिक होना चाहिए और उसमें किसी मौजूदा तकनीकी विचार की नकल नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न 76: पेटेंट पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क क्या होता है?
उत्तर:
पेटेंट पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो आवेदन की प्रकृति और आवेदक की श्रेणी (व्यक्ति, कंपनी, आदि) के आधार पर भिन्न हो सकता है।
प्रश्न 77: पेटेंट को रद्द (Revocation of Patent) करने का क्या प्रक्रिया है?
उत्तर:
पेटेंट को रद्द करने की प्रक्रिया में यह साबित करना होता है कि पेटेंट आवेदन प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी हुई थी या पेटेंट के तहत दावा किए गए आविष्कार में कोई खामी है। यह प्रक्रिया पेटेंट कार्यालय के समक्ष की जाती है और यदि सबूत सही पाए जाते हैं तो पेटेंट रद्द किया जा सकता है।
प्रश्न 78: पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन और उसके उपायों के बारे में विस्तार से बताएं।
उत्तर:
पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के पेटेंट आविष्कार का उपयोग करता है। इसके उपायों में न्यायालय में मामला दर्ज करना, मुआवजा प्राप्त करना, और व्यापारिक रोकथाम करना शामिल है। उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और पेटेंट मालिक को उचित संरक्षण प्राप्त होता है।
प्रश्न 79: ट्रेडमार्क पंजीकरण का क्या महत्व है?
उत्तर:
ट्रेडमार्क पंजीकरण का महत्व यह है कि यह किसी विशेष ब्रांड, उत्पाद या सेवा को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और उसकी कानूनी सुरक्षा करता है। पंजीकरण से व्यापारिक उल्लंघन रोका जा सकता है और व्यापार के लिए एक स्थिर पहचान स्थापित की जा सकती है।
प्रश्न 80: ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर क्या कानूनी उपाय होते हैं?
उत्तर:
ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ कानूनी उपायों में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करना, व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, मुआवजा प्राप्त करना और अन्य व्यापारिक कार्यवाही शामिल हैं।