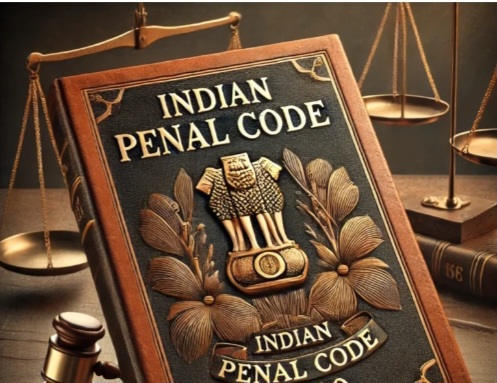– प्रथम सेमेस्टर –
प्रश्न 1. अपराध को परिभाषित कीजिए।
Define Crime.
उत्तर -भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोप अपराध होगा जिसके लिए दण्ड संहिता में दण्ड का प्रावधान है। वैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा अपराध को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है-
“अपराध विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध एवं लोकहित के लिए हानिकारक है।”
ब्लैकस्टोन के अनुसार, “अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है, जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो।”
स्टीफेन के अनुसार, “सम्पूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है।”
अतः अपराध के लिए कम से कम दो तत्वों का होना नितान्त आवश्यक है
(1) किसी कृत्य का किया जाना या किसी कृत्य का लोप (Omission), तथा
(2) दूषित आशय या दुर्भावना तथा इन कृत्यों या अपकृत्यों के लिए दण्ड विधि में दण्ड नियत होना चाहिए।
प्रश्न 2. अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए।
Discuss the essential elements of the Crime.
उत्तर- अपराध के आवश्यक तत्व- अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है-
(i) एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। तथा जो दण्ड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है;
(1) ऐसे मानव के मन में एक दुराशय है;
(iii) ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य;
(iv) ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या सम्पूर्ण समाज को एक क्षति
(1) मानव – किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दण्डनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए।
(2) दुराशय (Mens-rea) -“मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधीन हो। (Actus non facit reum nisi mens sit rea) अर्थात् कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन (आशय) वैसा न रहा हो।” इसी प्रकार “मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है।” (Actus meinvito factus non est mens actus) i
(3) आपराधिक कृत्य (Actus-reum)–किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते दण्डनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोप के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए।
(4) मानव को क्षति (Injury to human being)-क्षति किसी दूसरे किसी के शरीर या सम्पूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुँचायी गयी होनी चाहिए।
प्रश्न 3. अपराध किये जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं?
What are the different stages in the commission of a Crime?
उत्तर- किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना (Intevitable Accident) के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साशय एवं जानबूझकर किये गये अपराध को करने के लिए एक अपराधी सामान्यतया निम्न स्तरों (Stages) से होकर गुजरता है
(1) आशय (Intention);
(2) तैयारी (Preparation);
(3) प्रयास या प्रयत्न (Attempt);
(4) अपराध का निष्पादन (Execution) या क्रियान्वयन।
प्रश्न 4. आपराधिक मनःस्थिति ( दुराशय) से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Mens-rea?
उत्तर- दुराशय (Mens-rea) – दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य है द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय आंग्ल विधि का एक प्रसिद्ध सूत्र है (Actus: non facit reum nisi meres sit rea) कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषो नहीं बना देता है. जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो।
अत: यह स्पष्ट है कि दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति के पीछे कोई-न-कोई कारण होता है जो ऐसे आशय को जन्म देता है। दुराशय सामान्यत: अपराध के गठित होने की अनिवार्य शर्त है। दाण्डिक विधि की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार के अपराध को नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 5. जंगम सम्पत्ति को परिभाषित कीजिए।
Define Movable Property.
उत्तर – भारतीय संहिता की धारा 22 में ‘जंगम सम्पत्ति’ के विषय में बतलाया गया है। ‘जंगम सम्पत्ति’ शब्दों से यह आशयित है कि इनके अन्तर्गत हर भाँति की मूर्त सम्पत्ति आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें, जो भू-बद्ध हो या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में। जकड़ी हुई हों, इनके अन्तर्गत नहीं आतीं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सम्पत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई न हो, जिसे हटाया जा सकता हो, वे चल सम्पत्तीैया कहलाती हैं। जैसे- किताबें, जेवर, पंखे, बर्तन आदि।
प्रश्न 6. प्रयास को परिभाषित कीजिए।
Define ‘Attempt’.
उत्तर – प्रयास (attempt) प्रयास या प्रयत्न अपराध करने की दिशा में तृतीय चरण होता है तैयारी पूरी होने के पश्चात् अपराध का प्रयत्न प्रारम्भ होता है प्रयास या प्रयत्न (Attempt) आपराधिक कृत्य की दिशा में सीधा तथा प्रत्यक्ष कदम है। अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 1698 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रयत्न को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रयत्न का अपराध किया गया तब कहा जाता है जब उसका आशय कोई अपराध करना हो तथा उक्त आशय के साथ वह उस अपराध को करने की ओर अग्रसर होकर कोई कदम उठाए यह आवश्यक नहीं है कि अपराध पूर्णरूप से इसलिए कारित नहीं हो सका क्योंकि वह अपराधकर्ता के नियन्त्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों ने उसे पूरा नहीं होने दिया अर्थात् प्रयत्न के अन्तर्गत अपेक्षित परिणाम के प्राप्त करने का प्रयास सन्निहित है। किसी अपराध के लिए तैयारी कर लेने के पश्चात् उसे पूरा करने की ओर उन्मुख होना प्रयास या प्रयत्न कहलाता है।
प्रश्न 7. प्रयत्न कब दण्डनीय है?
When attempt is punishable?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दण्डनीय घोषित करती है। प्रयत्न अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम होता है। जब अपराधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है परन्तु कुछ कारणवश अर्थात् किसी बाह्य कारण से जो उसके है नियन्त्रण से परे था जिससे वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध करने का प्रयत्न किया है।
उच्चतम न्यायालय ने अभयानन्द मिश्र बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० (1961) एस० सौ० 1698 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न आरम्भ होता है एवं किसी कृत्य का किया जाना अपराध के निमित्त अगला कदम होता है जो सदैव दण्डनीय है।
प्रश्न 8. मात्र तैयारी कब दण्डनीय है?
When only Preparation is punishable?
उत्तर- तैयारी मात्र कब दण्डनीय है? (When only Preparation is punishable? – आशय तथा तैयारी सामान्य रूप से दण्डनीय नहीं है परन्तु निम्न परिस्थितियों में मात्र तैयारी (Preparation) दण्डनीय है
(1) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना; (धारा 122)
(2) भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना (धारा 126)
(3) कूट सिक्के (Counterfeit Coins) बनाने की तैयारी करना; (धारायें 233 235)
(4) डकैती की तैयारी करना (धारा 399 )
(5) आपराधिक षड्यन्त्र के अपराध के लिए तैयारी की पूर्वस्थिति आशय मात्र दण्डनीय है।
प्रश्न 9- अपराध और नैतिकता में क्या सम्बन्ध है?
What is the relation between Crime and Morality?
उत्तर- अपराध और नैतिकता में सम्बन्ध ऐसा माना जाता है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े होते हैं किन्तु यह एक आम धारणा है। विधि में मुख्यतया दण्ड विधि के अन्तर्गत समाविष्ट अपराध अनैतिक स्वरूप का होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक अपराध आवश्यक रूप से एक अनैतिक कृत्य होगा। परन्तु वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं है। दण्ड विधि के अन्तर्गत अपराध ऐसा कृत्य है जो दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं यह नैतिकता या अनैतिकता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दण्ड संहिता के अर्थान दण्डनीय अपराध माना गया है या नहीं। उदाहरण-गर्भपात करा देना अनैतिक कार्य होते हुए भी ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधि० 1971 के अधीन इसे वैधता प्राप्त है।
प्रश्न 10. सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य।
Act done in good faith.
उत्तर- सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य (Act done in good faith) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 52 के अनुसार, कोई बात ‘सद्भावपूर्वक’ की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।
इस धारा में दी गई परिभाषा नकारात्मक है अर्थात् कोई कार्य तब तक सद्भावपूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उचित सावधानी और ध्यानपूर्वक न किया गया हो।
पूनम वर्मा बनाम डॉ० अश्विनी पटेल, (1996) 4 एस० सो० 332 के बाद में ( उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई होमियोपैथिक चिकित्सक किसो रोगी का इलाज एलोपैथिक दवाइयों से करता है जिसके लिए वह अहं (Qualified) नहीं है ( और इसके परिणामस्वरूप रोगी और अधिक गम्भीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त होमियोपैथिक चिकित्सक का कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा अपितु उसे पोर असावधानी का दोषी माना जाएगा।
प्रश्न 11. अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? What do you understand by vicarious liability in crime?
उत्तर- अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व- आपराधिक विधि में साधारणतः आपराधिक दायित्व उसी व्यक्ति पर होता है जिसने वह अपराध कृत्य किया है न कि उसके बजाय या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को।
प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धान्त अपकृत्यों के लिए प्रायः लागू किया जाता है जिसके अन्तर्गत विशेष परिस्थिति में अपकृत्यकर्ता का दायित्व उसकी ओर से कोई अन्य तीसरा व्यक्ति वहन करता है, जैसे-सेवक के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व। परन्तु यह सिद्धान्त अपराध-विधि में लागू नहीं होता है। अतः अपराध के लिए सामान्यतः उसी को दण्डित किया जाता है जिसने अपराध कारित किया है न कि उसकी ओर से कि व्यक्ति को । । इंग्लैण्ड की दण्ड विधि में भी प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धान्त को नहीं अपन है। केवल अपवाद के रूप में निम्नलिखित दशाओं में सेवक द्वारा किये गये अपराध आपराधिक दायित्व उसके स्वामी पर होगा-
(i) सेवक द्वारा प्रकाशित किये गये अपलेख (Libel) के लिए आपराधिक उसके स्वामी पर होगा।
(ii) सार्वजनिक अपदू षण (Public Nuisance) के मामले में भी प्रतिनिि का सिद्धान्त लागू होगा।
प्रश्न 12. सहमति को परिभाषित कर इसे स्पष्ट कीजिए।
Define and Explain ‘Consent’.
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता में सहमति को परिभाषित नहीं किया गया संहिता में कई स्थानों पर सहमति शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। सहमति या विवक्षित हो सकती है। सहमति से आशय वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है, अ जोखिम उठाने को तैयार है यदि कोई अपहानि घटित होती है। सहमति से किये वो आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गयी है।
प्रश्न 13. प्रयत्न एवं तैयारी में क्या अन्तर है?
What is difference between Attempt and Preparation?
उत्तर- प्रयत्न एवं तैयारी में अन्तर
(Difference between Attempt and Preparation)
प्रयत्न and तैयारी
(1) प्रयत्न करना एक अपराध माना जाता
(1) तैयारी करना ही स्वयं में अपराध होता।
(2) प्रयत्न तब कहा जाता है जब किसी अपराध को करने की चेष्टा की जाती है। साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी है।
(2) किसी अपराध को करने के लिए साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी है
अपराध को करने की चेष्टा की जाती है। साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी है।
(3) संहिता अपराध करने के प्रयत्न को तैयारी दण्डनीय घोषित करती है।
(3) संहिता सामान्यतः अपराध की तैयारी करने को दण्डनीय अपराध नहीं घोषित करती।
प्रश्न 14. ( क ) कूटकरण ।
Counterfeiting.
(ख) सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि। Wrongful gain and wrongful loss.
उत्तर (क)-कूटकरण (Ccunterfeiting)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की चारा 28 में कूटकरण की परिभाषा दी गयी है। इसके अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीन के सदृश इस आशय से निर्मित करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि तदद्वारा प्रवेचना की जायेगी, वह ‘कूटकरण करता है। यह कहा जाता है।
धारा 28 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार, ‘कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो।
धारा 28 के स्पष्टीकरण (2) के अनुसार, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी ची के सदृश कर दे और सादृश ऐसा हो कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है से जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि व्यक्ति एक चीज की दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा प्रवचन करने का था या यह यह सम्भाव्य जानता था कि तदूद्वारा प्रवंचना की जायेगी।
उत्तर (ख)- सदोष अभिलाभ (Wrongful gain) – भारतीय दण्ड संहिक, 1860 की धारा 23 में सदोष अभिलाभ को परिभाषित किया गया है तथा साथ ही साथ ‘सदोष हानि’, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना भी परिभाषित किया गया है।
‘सदोष’ से तात्पर्य है किसी पक्षकार के विधिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालना।
जबकि सदोष अभिलाभ से तात्पर्य है
(1) किसी सम्पत्ति का अभिलाभ
(2) जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है।
(3) ऐसा अभिलाभ विधि प्राप्त साधनों से प्राप्त किया गया हो। सदोष अभिलाभ में सम्पत्ति को सदोष अर्जित करना तथा उसे सदोष रखे रहना दोनों ही शामिल हैं।
सदोष हानि (Wrongful loss)- सदोष हानि का अर्थ किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देना है तथा इसमें किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अवैध रूप से रखे रहना भी शामिल है। दूसरे शब्दों में सदोष हानि से तात्पर्य है
(1) किसी सम्पत्ति की हानि
(2) जिस व्यक्ति को सम्पत्ति की हानि हुई हो,
वह उसका वैध रूप से हकदार हो तथा हानि विधि-विरुद्ध साधनों से कारित होनी चाहिए।
प्रेमनाथ बनर्जी बनाम राज्य, (1866) 5 डब्ल्यू आर (क्रि०) 68 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधवा के बैलों को उसके मृतक पति द्वारा लिए गये ऋण की बसूली में बलपूर्वक गैर-कानूनी ढंग से छीन लिया जाना विधवा को हुई सदोष हानि माना गया है।
महालिगैया पुजारी बनाम राज्य, (1959) क्रि० लॉ ज० 881 के बाद में पोस्टमैन ने एक वी० पी० पार्सल का परिदान पाने वाले के पते पर न करते हुए उसकी रसीद पर स्वयं ही हस्ताक्षर करके पार्सल अपने पास रख लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पोस्टमैन द्वारा पार्सल स्वयं रख लेना सदोष अभिलाभ था क्योंकि पाने वाले के न मिलने की दशा में उसे पार्सल पोस्ट मास्टर को लौटा देना चाहिए था।
प्रश्न 15. सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by common intention?
उत्तर– सामान्य आशय सामान्य आशय से तात्पर्य है चित्त का मिलन, जब कई व्यक्तियों को किसी कार्य को करने में उस कार्य के आशय की जानकारी हो तो कहा जायेगा कि उनके चित्त का मिलन है। अतः सबका सामान्य आशय है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य अथवा जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
प्रश्न 16 कपटपूर्वक को परिभाषित कीजिए।
Define Fraudulently’.
उत्तर- कपटपूर्वक (Fraudulently)– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 25 में कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है। धारा 25 के अनुसार- कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।
रामचन्द्र गूजर बनाम सम्राट, (1937) 39 बम्बई लॉ रि० 1148 के वाद में कहा गया कि कोई कृत्य कपटपूर्वक है अथवा नहीं, यह जानने के लिए उस कृत्य को करने वाले व्यक्ति का आशय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशय का अनुमान प्राय: अभियुक्त के आचरण से लगाया जाता है।
डॉ० विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन, ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 1572 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ‘कपट’ में दो तत्वों का समावेश है- (1) धोखा, (2) जिस व्यक्ति के प्रति कपट किया गया है उसे क्षति। यह आवश्यक नहीं है कि क्षति आर्थिक ही हो। वह मानसिक, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित या अन्य किसी प्रकार की भी हो सकती है।
प्रश्न 17. स्वेच्छया । Voluntarily.
उत्तर- स्वेच्छया (Voluntarily)– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 39 में स्वेच्छया को परिभाषित किया गया है। धारा 39 के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को ‘स्वेच्छया’ कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना सम्भव है।
उदाहरण-‘पंकज’ लूट को आसान बनाने के उद्देश्य से एक बड़े शहर के रिहायशी मकान में रात को आग लगाता है और इस प्रकार उसके द्वारा लगाई गई आग के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ‘पंकज’ का आशय भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है तो भी यदि वह जानता था कि मकान में आग लगाने से यह सम्भव है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है।
ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम, ए० आई० आर० 1986 एस० सी० 1465 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों द्वारा अपनी झुग्गियाँ पब्लिक फुटपाथ पर बना लिए जाने को दण्ड संहिता की धारा 441 के सन्दर्भ में स्वेच्छया किया गया आपराधिक अतिचार नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें विवश होकर स्वयं की आजीविका के लिए ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।
प्रश्न 18 दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या अन्तर है? What is the difference between Document and Electronic Record?
उत्तर– दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर- (1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 29 दस्तावेज को परिभाषित करती है जबकि धारा 29 (क) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से सम्बन्धित है।
(2) दस्तावेज से तात्पर्य किसी ऐसे विषय से है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा या इनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा इस आशय से अभिव्यक्त या अंकित किया गया है ताकि उसका उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग होगा या उपयोग किया जाएगा।
बोरैया बनाम राज्य, 2003 क्रि० लॉ ज० 1031 (कर्नाटक) के वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शव परीक्षा रिपोर्ट (Post-mortem report) दस्तावेज है।
इसी प्रकार विभिन्न निर्णीत वादों में निम्नलिखित को दस्तावेज माना गया जैसे- (1) करेन्सी नोट, (2) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कर निर्धारण का आदेश (3) विदेश में किये गये टेलीफोन काल्स के लिए टेलीफोन आपरेटर द्वारा तैयार की गई किराया-रसीद, (4) वृत्तचित्र आदि।
जबकि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 29 (क) में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है जो सन् 2000 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है इसके जोड़ने के पीछे संसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का पारित होना है अतः जब ऐसे आंकड़े, अभिलेख या आंकड़े जनित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचित, प्राप्त या प्रेषित किए गए प्रतिबिम्ब, ध्वनि या माइक्रो-फिल्म या कम्प्यूटर जनित माइक्रोचिप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अन्तर्गत आते हैं। इसी प्रकार अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाता है।
प्रश्न 19 तथ्य की भूल कब क्षम्य है? स्पष्ट करें।
When the mistake of fact is excusable?
उत्तर -भारतीय दण्ड संहिता की धारा 76 तथा धारा 79 दोनों तथ्य की भूल के बचाव का उल्लेख करती हैं। इन दोनों धाराओं में मुख्य अन्तर यह है कि धारा 76 में कार्य करने वाला व्यक्ति तथ्य की भूल के अन्तर्गत यह समझता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य है अर्थात् यह समझता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है (bound by law) जबकि धारा 79 के अन्तर्गत बचाव का दावा करने वाला व्यक्ति तथ्य की भूल के अन्तर्गत सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए विधि के अन्तर्गत प्राधिकृत था अर्थात् प्रश्नगत कार्य करना विधित: औचित्यपूर्ण (न्यायानुमत- Justified) था अर्थात् (Justified by law) था। दोनों धाराओं में कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय सद्भावपूर्वक होना चाहिए।
इस प्रकार धारा 76 के अन्तर्गत तथा धारा 79 के अन्तर्गत बचाव का सहारा लेने वाले व्यक्ति को निम्न बातें साबित करनी होंगी-
(1) यह कि वह तथ्य की भूल के अन्तर्गत कार्य कर रहा था।
(2) यह कि वह तथ्य की भूल के अन्तर्गत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता था कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य था। (धारा 76) या प्रश्नगत कार्य करना उसके लिए उचित या विधिपूर्ण था जिसे करने की अनुमति उसे विधि के अन्तर्गत प्राप्त थी। (धारा 79)
प्रश्न 20. विधि की भूल क्षम्य नहीं है।
Mistake of law is not excusable?
उत्तर-विधि की भूल क्षम्य नहीं है- विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है (Ignorance of law is no excuse)। प्रत्येक नागरिक से देश की विधि की जानकारी की अपेक्षा की जाती है। यदि विधि की भूल को भी आपराधिक दायित्व से बचाव के रूप में स्वीकार किया जाए तो प्रत्येक अभियुक्त केवल इसी बचाव की माँग करेगा तथा न्यायालय के लिए यह निर्धारित करना कठिन हो जाएगा कि अभियुक्त को वास्तव में विवादित मामले से सम्बन्धित विधि की जानकारी थी अथवा नहीं। अतः कोई कार्य करते समय व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह यह जानकारी प्राप्त कर ले कि उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी प्रचलित विधि के विरुद्ध तो नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो यह उसकी असावधानी होगी जिसके लिए उसे दण्ड भुगतना होगा।
प्रश्न 21 दुर्घटना।
Accident.
उत्तर- दुर्घटना (Accident)- दुर्घटना को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कार्य है जो अनियोजित, अप्रत्याशित या अकल्पित हो।
स्टीफेन महोदय ने दुर्घटना को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसा कृत्य जो बिना आशय के किया गया हो तथा जिसका ऐसा परिणाम हो जिसकी कल्पना उस परिस्थिति में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उचित सावधानी व सतर्कता बरतते हुए कभी नहीं करेगा।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 80 दुर्घटना पूर्ण कार्य को एक बचाव के रूप में मान्यता देती है ।
एक कार्य को दुर्घटना का परिणाम तब माना जायेगा जब उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व (Essential Ingredients) हों।
(1) वह कृत्य आकस्मिक रूप से दुर्घटनावश या दुर्भाग्य से कारित हुआ हो,
(2) वह कार्य आपराधिक आशय या जानकारी के बिना किया गया हो,
(3) वह कार्य ऐसे कार्य का परिणाम हो जो वैध रूप से वैध साधनों द्वारा किया गया हो,
(4) वह कार्य उचित सावधानी तथा सतर्कता के साथ किया गया हो।
शाकिर खान बनाम क्राउन, ए० आई० आर० 1931 लाहौर 54 नामक बाद में शिकारियों का एक दल शिकार पर गया। शाकिर खान भी उस दल का सदस्य था। एक जानवर को मारते समय गोली जानवर को न लग कर पार्टी के एक सदस्य के पैर को बेध गई न्यायालय ने इस कृत्य को एक दुर्घटना माना तथा अभियुक्त को धारा 80, भा० द० सं० का बचाव स्वीकार किया।
प्रश्न 22 शिशु का आपराधिक दायित्व।
Criminal Liability of Child.
उत्तर- शिशु का आपराधिक दायित्व (Criminal Liability of Child) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार, “कोई भी बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की गयी हो। यह माना जाता है कि सात वर्ष से कम आयु का बच्चा अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझता उसे अक्षम गुड़िया (Doli-incapax) माना जाता है। अतः वह उसके परिणामों के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सात साल से कम उम्र के शिशु पर यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके उत्तर में यह पर्याप्त होगा कि वह सात वर्ष से कम है। धारा में प्रयुक्त शब्दावली ‘सात वर्ष से कम’ विवाद का विषय रही है। क्योंकि इसके बाद वाली धारा 83 सात साल के ऊपर के शिशुओं के सम्बन्ध में उपबंध करती है। न्यायालयों और विद्वानों का अब यह निश्चित मत है कि ‘सात साल से कम’ शब्दावली से तात्पर्य ‘सात साल तक’ से है क्योंकि दण्ड-विधि के अन्तर्गत निर्णय का यह मान्य सिद्धान्त है कि सन्देह का लाभ सदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिये।
धारा 83 के अनुसार, “कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से ऊपर तथा बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जो समझ की परिपक्वता के अभाव में अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ हो।” धारा 82 में जहाँ शिशु को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है वहीं धारा 83 के अन्तर्गत यह उन्मुक्ति सशर्त बता दी गई है, अर्थात् सात साल से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम उम्र का शिशु भी आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जा सकता है, यदि यह साबित कर दिया जाये कि उसमें पूर्णतया समझने की शक्ति का अभाव थां, यानि वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में पूर्णतया असमर्थ था।
वस्तुत: धारा 82 तथा 83 दोनों के ही प्रावधान सुधारात्मक हैं, दण्डात्मक नहीं जिनका मुख्य उद्देश्य बालकों को सुधारने का अवसर प्रदान करना है। यह बात कृष्ण भगवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए० आई० आर० 1989 पटना 217 के बाद में कही गयी है।
प्रश्न 23. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 में वर्णित सहमति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, सम्बन्धी विधि की विवेचना कीजिए।
Discuss the law relating to consent known to be given under fear or misconception in Section 90 of I.P.C.
उत्तर- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 में स्वतन्त्र सहमति से सम्बन्धित बातों का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्वतन्त्र सहमति से तात्पर्य यह है कि ऐसी सहमति जो बिना किसी प्रकार के कपट अथवा भय के दी गई हो। पारा 90 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनमें सहमति को ‘स्वतन्त्र सहमति’ नहीं माना गया है, अत: इनके आधार पर किसी अपराध से बचाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से कोई हो सकती है-
(1) किसी भय के अधीन दी गई सहमति (2) किसी तथ्य के भ्रम के कारण दी गई सहमति या कपट द्वारा ली गई सहमति: (3) विकृत-चित्त द्वारा दी गई सहमति (4) 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई सहमति तथा (5) अस्वैच्छिक मतता के अधीन दी गई सहमति।
दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1958 पटना 190 के मामले में अभियुक्त हाईस्कूल की परीक्षा में लगातार तीन बार फेल होता रहा। अतः उसने अपनी आत्महत्या कर लेने का निश्चय अपनी 19 वर्षीया शिक्षित पत्नी को बताया। इस पर पत्नी ने उससे कहा कि स्वयं की आत्महत्या करने के पहले वह उसका (पत्नी का) जीवन समाप्त करे बाद में स्वयं आत्महत्या करे यह तय हो जाने पर अभियुक्त ने अपनी पत्नी की जान ले ली परन्तु स्वयं आत्महत्या करने के पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने पत्नी की सहमति का बचाव प्रस्तुत किया, किन्तु न्यायालय ने अभियुक्त के बचाव को निरस्त करते हुए कहा कि पत्नी ने अपनी सहमति भय के अधीन दी अतः उसे धारा 90 का संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वह सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है, का दोषी होगा।
अभिप्रेत है
प्रश्न 24. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 88, 89 एवं 92 के अधीन फायदा से क्या अभिप्रेत है?
What is meant by ‘Benefit’ under Section 88, 89 and 92 of the Indian Penal Code?
उत्तर- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 88 89 एवं 92 ये तीनों धारायें किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति एवं सम्मति के बिना सद्भावनापूर्वक किये गये कार्य से सम्बन्धित हैं।
विधि का सामान्य नियम यह है कि जानबूझकर कारित की गई मृत्यु के लिए सम्मति का बचाव नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि कोई कृत्य सद्भावनापूर्वक सम्मति देने वाले व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया है, तो उस दशा में यदि सम्मति देने वाले की मृत्यु भी कारित हो जाए, तो भी वह धारा 88 के अन्तर्गत क्षम्य होगी जैसा कि धारा में दिये गये दृष्टान्त से ही स्पष्ट है कि यदि कोई शल्य चिकित्सक (Surgeon) सद्भावनापूर्वक किसी मरीज को बीमारी ठीक करने के लिए मरीज की स्वतन्त्र सहमति से, कोई खतरनाक ऑपरेशन करता है, जो अधिकांशतः घातक ही सिद्ध हुआ है, और ऑपरेशन के परिणामस्वरूप उस मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में उस चिकित्सक को अपराधी मानकर दण्डित नहीं किया जा सकेगा।
इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति जो किसी जंगली जानवर के हमले से जूझ रहा है, पास खड़े अपने मित्र को उस जंगली जानवर पर गोली चलाने के लिए कहता है, यद्यपि वह जानता है कि गोली से उसे स्वयं भी खतरा हो सकता है, तो ऐसी दशा में मित्र द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मित्र को हत्या के लिए दोषी नहीं माना जाएगा।
इसी प्रकार धारा 89 के अन्तर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बालकों अथवा विकृतचित व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनके फायदे के लिए किये गये कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया। गया है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द ‘फायदा’ से आशय आर्थिक लाभ से नहीं है और न संरक्षक को होने वाले लाभ से है। फायदा बालक या विकृत्त-चित्त से हित में हो या लौकिक (Temporal) स्वरूप का हो। दण्ड विधि के निर्माताओं ने से निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया है-
(1) एक अभिभावक (माता या पिता) अपने बच्चे को एक मर्यादित सीमा में रहते हुए मारता है ताकि वह सुधर जाए, जहाँ अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है।
(2) ‘अ’ अपने बच्चे के हित के लिए उसे परिरोध में रखता है, ‘अ’ ने कोई अपराध नहीं किया है।
धारा 88 89 तथा धारा 92 का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को सद्भावपूर्वक किये गये चिकित्सीय कृत्यों के लिए आवश्यक संरक्षण दिलाना है, प्रस्तुत धारा 92 के दृष्टान्त (क) तथा (ख) में जो उदाहरण दिया गया है उनमें ‘सम्मति’ दी जाना असम्भव है तथा दृष्टांत (ग) एवं (घ) में वर्णित उदाहरण में विधिक सम्मतिः का अभाव है। फिर भी उक्त चारों परिस्थितियों में अभियुक्त का कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा।
प्रश्न 25. सद्भावनापूर्वक दी गई संसचूना सम्बन्धी विधि की विवेचना करें।
Discuss the law relating to communication made in good Jaith.
उत्तर- सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 93 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को दण्डित होने से संरक्षण प्रदान किया गया है जो किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक, उस व्यक्ति के हित के लिए सूचना देता है और ऐसी सूचना के कारण उस व्यक्ति को कोई अपहानि हो जाती है। इस धारा का प्रयोग प्रायः चिकित्सकों द्वारा रोगी की सम्भावित मृत्यु के बारे में सूचना दिये जाने के प्रकरणों में लागू होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई डॉक्टर कैंसर जैसे-गम्भीर रोग से पीड़ित किसी रोगी को सद्भावना से यह सूचना देता है कि उसकी राय में वह दो-चार महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा और इस सूचना से रोगी को मानसिक आघात पहुंचाता है और वह मर जाता है, तो ऐसी दशा में । डॉक्टर को रोगी की मृत्यु के लिए दोषी नहीं माना जायेगा।
प्रश्न 26 हेतुक । Motive.
उत्तर- हेतुक का अर्थ (Meaning of Motive) — हेतुक या प्रेरणा वह बल है जो किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य करने हेतु चलायमान या गतिशील करती है। हेतुक या प्रेरणा का स्थान व्यक्ति का मस्तिष्क होता है और यही हेतुक (Motive) या प्रेरणा व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश या प्रेरित करती है। किसी कार्य की प्रेरणा या हेतुक को उत्पन्न करने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाना, बदला लेने की भावना, किसी से अवैध या दूषित सम्बन्ध किसी के प्रति कर्ण या अन्य दायित्वों से छुटकारा प्राप्त करने का दबाव या किसी बुरी (दूषित) मनोदशा को पूर्ण करना आदि महत्वपूर्ण होते हैं। अपराध का हेतुक जितना अधिक प्रबल तथा सुनिश्चित होगा, दण्ड भी उतना ही अधिक कठोर होगा। यदि आपराधिक हेतु या उद्देश्य अधिक प्रबल न हो और अपराध उत्तेजनावश किया गया हो तो स्वाभाविक रूप से दण्ड तुलनात्मक दृष्टि से कम कठोर स्वरूप का होगा।
प्रश्न 27. तुच्छ कार्य। Trifling Act.
उत्तर- तुच्छ कार्य (Trifling Act) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य करने सम्बन्धी प्रावधान करती है। इस धारा के उपबन्ध लेटिन सूत्र ‘de minimis non curat lex’ पर आधारित है, जिसका अर्थ है, “विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती तात्पर्य यह है कि विधि ऐसी छोटी-मोटी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देती जो शाब्दिक अर्थ में तो अपराध की कोटि में आते हैं लेकिन उनसे क्षति या हानि नाममात्र की होती है, जिनके लिए अपराध का संज्ञान करना भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
इस धारा के उपबन्ध के सम्बन्ध में दण्ड संहिता के निर्माताओं ने कहा है कि भाषा को अपूर्णता के कारण ऐसे अनेक कृत्य हैं जो शाब्दिक दृष्टि से किसी अपराध के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु यदि वास्तव में देखा जाए तो उनके पीछे आपराधिक भावना नहीं रहती है, अतः उन्हें अपराध मानना जनहित में नहीं होगा। उदाहरणार्थ, किसी दूसरे व्यक्ति के दवात में कलम डुबोना चोरी का अपराध है, किसी व्यक्ति के पास से तेज रफ्तार में कार से धूल उड़ाते हुए गुजरना रिष्टि है, किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठने के लिए अन्दर करना चोट है, लेकिन क्या इनके लिए आपराधिक कार्यवाही चलाना न्यायोचित होगा? यदि ऐसी छुट-पुट बावों को अपराध मानकर लोगों को दण्डित किया जाने लगे, तो समाज में लोगों का साथ-साथ रहना दूभर हो जाएगा। इसी कारण ऐसे नगण्य क्षतिकारक कृत्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है।
प्रश्न 28. विकृतचित्त वाले व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है?
What is Rights to Private defence against the act of a person of unsound mind.
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय विकृतचित्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह विकृतचित्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि-विरुद्ध है, जानने में असमर्थ है।
धारा 84 के लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपराध कार्य करने के समय विकृतचित्त हो। पहले अथवा बाद की विकृतचित्तता बचाव का आधार नहीं हो सकती। अपराध कार्य किये जाने के समय व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी थी, इसका निर्धारण वाद की परिस्थिति व अभियुक्त के आचरण के आधार पर किया जा सकता है। यदि अभियुक्त को तरफ से यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध-कार्य किये जाने के समय वह विकृतचित तो धारा 84 का बचाव प्रदान किया जा सकेगा।
प्रश्न 29. विधिक उत्पत्तता एवं चिकित्सीय उन्मत्तता में क्या अन्तर है?
What is the difference between Legal Insanity and Medical Insanity?
उत्तर-विधिक उन्मत्तता एवं चिकित्सीय उन्मत्तता में अन्तर – विधिक विकृतचित्तता (पागलपन) के अन्तर्गत वे ही पागलपन आते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने द्वारा किये जाने वाले कृत्यों की प्रकृति को समझने की क्षमता नहीं रखता है, और यदि वह इसे समझता भी है, तो यह नहीं जानता कि इसका कृत्य अनुचित अथवा विधि-विरुद्ध है या नहीं। जबकि धारा-84 के अन्तर्गत चिकित्सीय विज्ञान को ज्ञात सभी प्रकार के पागलपन नहीं आते हैं।
विधिक विकृतचित्तता के लिए दण्ड संहिता में ‘मस्तिष्कीय अस्वस्थता’ पदावली का प्रयोग हुआ है न कि पागलपन का अतः मात्र मस्तिष्कीय अस्वस्थता ही बचाव नहीं है, अपितु इसे ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति का निर्णय या विवेक प्रभावित हो जबकि चिकित्सकीय विकृतचित्तता केवल इसमें पागलपन को ही दर्शाना होता है अत: इसमें अनेकों प्रकार के पागलपन आते हैं। अत: चिकित्सीय दृष्टिकोण के अनुसार अपराध कारित करते समय हर व्यक्ति पागल होता है अतः उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिलनी चाहिए।
प्रश्न 30. एक व्यक्ति मत्तता के प्रभाव में अपराध कारित करता है। क्या वह कोई बचाव ले सकता है? सम्बन्धित विधि का वर्णन कीजिए।
A Person commits a crime under the influence of drunkenness. Can he take any defence? Discuss the Law.
उत्तर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परन्तु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसको नशा हुआ है, उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गयी थी।” अर्थात् धारा 85 केवल उसी समय बचाव प्रदान करती है जबकि मत्तता उस व्यक्ति की इच्छा का परिणाम न हो अर्थात् यदि मत्तता उस व्यक्ति को स्वयं की इच्छा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है तो उसे दायी ठहराया जा सकता है। कोई मतता स्वैच्छिक है या अस्वैच्छिक, इसका मापदण्ड धारा 85 में ही उपबन्धित किया गया है। यदि वह वस्तु जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को नशा होता है, उस व्यक्ति के ज्ञान के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है तो वह नशा अस्वैच्छिक माना जायेगा। जैसा कि पहले कहा गया है कि ज्ञान के बिना कोई वस्तु दी गयी तब मानी जायेगी जब दबाव या भय दिखाकर दी गयी हो। स्वैच्छिक मत्तता या अस्वैच्छिक मत्तता को निर्धारित करने का कोई निश्चित सिद्धान्त स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती हैं, ऐसी हालत में अपराधी का दायित्व निर्धारित करना और भी कठिन हो जाता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यदि अपराध करते समय अभियुक्त की मत्तता उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न हुई थी, तो भले ही आंशिक रूप से उस मनता में उसकी अनिच्छा रही हो, फिर भी उत्पन्न हुई थी। उसे दायी ठहराया जा सकेगा। इस प्रकार धारा 85 के अन्तर्गत केवल अस्वैच्छिक मत्तता का ही बचाव स्वीकार किया गया है। एम्परर बनाम नागसेन, ए० आई० आरe 1939 रंगून 16; रामशंकर बनाम स्टेट ऑफ एम० पी० ए० आई० आर० 1981 एस० सी० 644 के बाद में कहा गया कि स्वैच्छिक मत्तता किसी भी हालत में बचाव प्रदान नहीं कर सकती यद्यपि इसके आधार पर दण्ड में कमी की जा सकती है।
प्रश्न 31. कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है?
When the right of private defence of property extends to causing death?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 103 में यह बताया गया है कि कब सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 103 के अनुसार- सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का अवसर तब आता है। जब दोषकर्ता निम्नलिखित अपराधों में से किसी भी भाँति के अपराध में आता हो किन्तु शर्त यह है कि इस अधिकार का प्रयोग करने वाले को धारा 99 की सीमा के अन्दर रहते हुए कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित अपराध ये हैं –
(1) लूट; (2) रात्रि गृह भेदनः
(3) अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गई है, जो मानव आवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है;
(4) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।
प्रश्न 32 आवश्यकता। Necessity.
उत्तर- आवश्यकता (Necessity)- आवश्यकता के कार्य (Act of Necessity) अपकृत्य तथा आपराधिक विधि में एक सफल बचाव या प्रतिवाद (defence) है। इस शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे कार्यों के फलस्वरूप होने वाली क्षति के लिए दायित्व से बचाव का प्रावधान है जो परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक है। इस बचाव या अपवाद (Exception) के पीछे सिद्धान्त यह है कि यदि कोई बड़ी हानि को बचाने के लिए कोई छोटी क्षति या हानि कारित की जाती है तो ऐसा क्षति करने वाला उन्मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। भले ही वह यह जानता हो कि जो कार्य वह करने जा रहा है, वह अपराध है। लोकहित ही सर्वोपरि विधि है “Sallus populi Est Suprema lex” यह सूक्ति भी आवश्यकता के कार्य को बचाव के रूप में मान्यता देने का समर्थन करती है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के कार्य को बचाव (Exception) के रूप में मान्यता देती है। धारा 81 के अन्तर्गत यदि चरम आपात स्थिति में कोई हानि कारित किया जाना अनिवार्य या आवश्यक हो जाय तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि हानि कम से कम हो। इसी प्रकार यदि एक बेहोश, पायल व्यक्ति की शल्यक्रिया करना आवश्यक हो तो उसकी सहमति या उसके संरक्षण या रिश्तेदारों की तलाश किये बिना उसकी शल्यक्रिया की जा सकती है तथा यह कार्य शल्यक्रिया करने वाले पर किसी दायित्व को अधिरोपित नहीं करेगा।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 के अन्तर्गत आवश्यकता के बचाव के निम्न आवश्यक तत्व है –
(i) आवश्यकता के अन्तर्गत किया गया कृत्य आपराधिक मनःस्थिति के या दुराशय के बिना किया गया होना चाहिए, भले ही वह कार्य करने वाला यह जानता था कि जो कार्य वह कर रहा है, वह अपराध है;
(ii) कृत्य सद्भावपूर्वक (In good faith) किया गया हो;
(iii) कृत्य करने के पीछे आशय किसी बड़ी हानि से बचाने का (iv) जिस बड़ी हानि से बचाने के आशय से कृत्य किया गया था वह शरीर या सम्पत्ति से सम्बन्धित होनी चाहिए।
विशम्भर बनाम रुमल, ए० आई० आर० 1951 इलाहाबाद 500 नामक वाद में अभियुक्त जो ग्राम-सरपंच था, ने एक व्यक्ति का मुँह काला कर जूतों से पीटते हुऐ गाँव में घुमाने का आदेश दिया। उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 तथा 506 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया गया। उसने अपने बचाव में कहा कि उस व्यक्ति ने एक हरिजन लड़की को छेड़ा था तथा गाँव में लगभग 200 लोग लाठी-डण्डे लेकर उस व्यक्ति को मारने के लिए उद्यत थे। उसका मुँह काला कर जूतों से पीटने का आदेश बिना किसी दुराशय के दिया गया था तथा परिवारीगण की जान बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। न्यायालय ने परिस्थितियों के अनुसार अभियुक्त ग्राम सरपंच के आदेश को उचित ठहराया तथा यह निर्णय दिया कि उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 81 के अन्तर्गत आवश्यकता का बचाव उपलब्ध था।
प्रश्न 33. विधि विरुद्ध जमाव को स्पष्ट कीजिए।
Explain an Unlawful Assembly.
उत्तर-विधि विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly)- विधि विरुद्ध जमाव लोक-शान्ति के विरुद्ध अपराध है। यहाँ व्यक्तियों के ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को अपराध माना गया है जो लोकशान्ति को भंग करने के लिए एकत्र हुआ हो। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 के अन्तर्गत दी गई है
इस परिभाषा के अनुसार, “पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को जिसका उद्देश्य इस धारा में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जायेगा। ” इस धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट कहता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं है, बाद में विधि विरुद्ध हो जायेगा। विधि विरुद्ध जमाव स्वयं एक अपराध है चाहे जमा हुए व्यक्तियों ने कोई कृत्य किया हो या नहीं।
प्रश्न 34. दुष्प्रेरण का क्या अर्थ है?
What is meaning of Abatements?
उत्तर- दुष्प्रेरण (Abetment)-रण का अर्थ है ‘उकसाना’ या ‘प्रोत्साहित करना। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करके दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने हेतु उकसाता है या प्रोत्साहित करता है तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है तथा उसके कार्य को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण अपने आप में अपराध नहीं है परन्तु यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है या प्रोत्साहित करता है तो उसका उत्प्रेरण दुष्प्रेरण हो जाता है तथा ऐसा करना एक अपराध माना गया है।
प्रश्न 35. दुष्प्रेरक किस सीमा तक मुख्य अपराधी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है?
To what extent is an abettor liable for an act committed by a Principal accused?
उत्तर- दुष्प्रेरक का दायित्व भारतीय दण्ड संहिता के दुष्प्रेरण के अध्यायों में धारा 109 से 120 तक दुष्प्रेरक के दायित्व का वर्णन किया गया है। धारा 109 के अनुसार यदि कोई कार्य दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए भारतीय दण्ड संहिता में अलग से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है तो दुष्प्रेरक को उसी दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है। जैसे ‘ख’ को जो एक लोक सेवक है, ‘ख’ के पदीय कृत्यों के प्रयोग में ‘क’ पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए लोक सेवक है, ‘ख’ के पदीय कृत्यों के प्रयोग में ‘क’ पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्थापना करता है। ‘ख’ वह रिश्वत प्रतिग्रहीत कर लेता है। ‘क’ ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है।
प्रश्न 36 कब दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है?
When the abatement of an abatement is an offence?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार किसी अपराध का दुष्प्रेरण अपराध है इसलिए ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। जैसे-‘क’, ‘ख’ को ठकसाता है कि वह ‘ग’ को उकसाकर ‘घ’ की हत्या करा दे। ‘क’ के उकसाने पर ‘ख’, ‘ग’ को ‘घ’ की हत्या के लिए उकसाता है। ‘ग’, ‘घ’ की हत्या कर देता है। ‘क’ और ‘ख’ दोनों दुष्प्रेरक होने के कारण दण्ड के भागी हैं।
इस स्पष्टीकरण के अनुसार एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप द्वारा स्वयं को दुष्प्रेरक की कोटि में ला खड़ा कर सकता है, भले ही उसमें तथा अपराध कार्य के लिए नियोजित अपराधी में किसी प्रकार का सीधा सम्पर्क न हो। हरियाणा राज्य बनाम वजीर चंद, ए० आई० आर० (1989) सु० को ० 378 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ससुराल में बहू द्वारा आत्महत्या के मामले में यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसे ससुराल वालों ने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया होगा।
प्रश्न 37. लोक अपदूषण। Public Nuisance.
उत्तर- लोक अपदूषण (Public Nuisance) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 लोक अपदूषण अथवा लोक उपताप (Public Nuisance) की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार लोक अपदूषण कोई ऐसा कार्य या अवैध लोप है जिससे जनसाधारण को ले आसपास रहते हो या आसपास की सम्पत्ति पर कब्जा रखते हों, कोई सामान्य क्षीत, सकर (खतरा) या क्षोभ (खीझ) उत्पन्न होती है या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होन अवश्यम्भावी हो।
प्रश्न 38 लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों से क्या अभिप्रेत है? What is meant by offences against Public Tranquillity?
उत्तर- लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध-ऐसे कृत्यों को दण्डनीय अपराध माना गया है जो लोक शांति को भंग करते हैं या जिनसे समाज की शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्तियों के ऐसे विधि-विरुद्ध जमाव को अपराध माना गया है जो लोक शांति को भंग करने के लिए एकत्र हुआ हो। इस प्रकार के अवैध जमाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दण्डित किये जाने की व्यवस्था है, भले ही वास्तविक रूप से अपराध कृत्य उनमें से किसी एक या कुछ व्यक्तियों ने ही किया हो। लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों में विधिविरुद्ध जमाव, बल्वा, दंगा एवं विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना प्रमुख है।
प्रश्न 39. राजद्रोह के अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं?
What are the necessary ingredients for fedition?
उत्तर- संहिता की धारा 124 (क) के अनुसार- जो कोई व्यक्ति बोले गये, लिखे गये या संकेतों अथवा दृश्रूपणों द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमान या अप्रीति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है तो उसे इस धारा के अन्तर्गत राजद्रोह के लिए दण्डित किया जायेगा। अतः राजद्रोह के अपराध के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि अभियुक्त द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या अप्रीति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय। अप्रीति का अर्थ शत्रुता की भावना उत्पन्न करने से है। इसके अन्तर्गत सरकार की आलोचना सम्मिलित नहीं है चाहे वह कितनी ही कटु क्यों न हो।
प्रश्न 40. आपराधिक षड्यन्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Write a short note an Criminal Conspiracy.
उत्तर- आपराधिक षड्यन्त्र – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-क में दी गई परिभाषा के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति (1) कोई अवैध कार्य या (2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यन्त्र कहलाती है। परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यन्त्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। उद्देश्य तत्वहीन है।
प्रश्न 41. बल्वा एवं दंगा को परिभाषित कीजिए।
Define Rioting and Affray.
उत्तर- बल्वा (Rioting)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 146 में बल्वा को परिभाषित किया गया है। धारा 146 के अनुसार- “जब विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के लिए दोषी होता है।”
दंगा (Affray) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है धारा 159 के अनुसार-“जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक-शान्ति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वह ‘दंगा’ करते हैं।”
दंगा (affray) शब्द फ्रेंच भाषा के Affraier शब्द से बना है जिसका अर्थ है, आतंकित करना यानि जनता को आतंकित करना।’
दंगा के अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं –
(1) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई,
(2) लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो,
(3) उनकी लड़ाई से लोकशान्ति को व्यवधान पहुँचे।
प्रश्न 42 आपराधिक बल एवं हमला में क्या अन्तर है?
What is the difference between criminal force and assault?
उत्तर- आपराधिक बल एवं हमला में अन्तर –
आपराधिक बल प्रयोग
(1) आपराधिक बल प्रयोग में अपराधी किसी अन्य व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है।
(2) आपराधिक बल प्रयोग हमले की अपेक्षा अधिक उत्तेजक एवं गम्भीर होते हैं।
(3) आपराधिक बल प्रयोग में हमला सम्मिलित होता है ।
हमला (Assault)
(1) हमले में अपराधी अपने हावभाव, तैयारी या धमकी से अन्य व्यक्ति के मन में आपराधिक बल प्रयोग की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है।
(2) हमला आपराधिक बल प्रयोग की – पूर्व अवस्था है।
(3) हमले में आपराधिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं होता।
प्रश्न 43. बल्वा एवं दंगा में क्या अन्तर है?
What is difference in Riot and Affray?
उत्तर – बल्चा तथा दंगा दोनों ही शान्ति के विरुद्ध अपराध हैं। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा का अपराधी होगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोकस्थानों में लड़कर लोकशान्ति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं –
बल्वा (Riot)
(1) बल्वा निजी या सार्वजनिक (Private or Public) स्थान पर हो सकता है।
(2) बल्वा के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम पाँच होनी आवश्यक है।
(3) बल्वा में विधि-विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दण्डित किया जाता है, भले ही उसके कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो। न
(4) बल्वा दंगे की अपेक्षा अधिक गम्भीर अपराध होने के कारण उसके लिए दो वर्ष का सादा या कठोर कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।
दंगा (Affray)
(1) दंगा सिर्फ सार्वजनिक स्थान (Public Place) पर ही किया जा सकता है, निजी स्थान पर नहीं।
(2) दंगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
(3) दंगे में सिर्फ वे ही व्यक्ति दण्डित होते हैं जिन्होंने वास्तव में उसमें भाग लिया हो।
(4) दंगा अपेक्षाकृत कम गम्भीर अपराध है, अत: उसके लिए सिर्फ एक मास तक का सादा या कठोर कारावास या एक सौ रुपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है?
प्रश्न 44. बल्वा एवं विधि विरुद्ध जमाव में क्या अन्तर है? What is difference between Riot and Unlawful Assembly?
उत्तर- बल्वा एवं विधि-विरुद्ध जमाव (Riot and Unlawful Assembly) –
बल्वा ( धारा 146)
(1) यदि दोनों पक्ष उपद्रवी ढंग से एकत्रित होते हैं तथा अपने उद्देश्य को हिंसा द्वारा यथार्थतः निष्पादित करते हैं तो यह एक बल्वा होगा।
(2) बल्वा में हिंसा या बल • प्रयोग आवश्यक है।
(3) बल्वा का क्षेत्र सीमित है इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 146 में परिभाषित किया गया है।
विधि-विरुद्ध जमाव (धारा 141 )
(1) यदि व्यक्तियों का समूह यानि कम से कम 5 से अधिक व्यक्ति एक प्रयोजन वश केवल मिलते हैं जिसे यदि सम्पादित किया जाता तो वे बल्वाकारी बन जाते तथा बिना कुछ किये और प्रयोजन को निष्पादित किये ही बिखर जाते हैं तो यह एक विधि-विरुद्ध जमाव माना जायेगा।
(2) विधि-विरुद्ध जमाव में अवैध उद्देश्य ही पर्याप्त है बल या हिंसा आवश्यक नहीं है।
(3) विधि-विरुद्ध जमाव का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है तथा इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है।
प्रश्न 45 घोर उपहति । Grievous hurt.
उत्तर- घोर उपहति (Grievous Hurt)– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 घोर उपहति को परिभाषित करती है। उपहति (चोट) की निम्नलिखित किस्में ही घोर उपहति कहलाती हैं जो इस प्रकार हैं –
(1) पुंसत्वहरण
(2) दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद
(3) दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद
(4) किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद
(5) किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास
(6) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपोकरण
(7) अस्थि या दाँत का भंग या विसंधान
(8) कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण चोटिल व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को करने के लिए असमर्थ रहता है।
प्रश्न 46. ‘अ’ एक महिला का घूंघट साशय हटा देता है। क्या ‘अ’ किसी अपराध के लिए दायी है? ‘A’ intentionally pulls up a women’s veil. Whether ‘A’ is liable for any offence?
उत्तर –यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का घूँघट साशय हटा देता है तो ये कृत्य उस महिला की सहमति के बिना तथा भय या क्षोभ (खीझ) उत्पन्न करने वाले होने के कारण धारा 350 के अन्तर्गत आपराधिक बल प्रयोग करने का अपराध का दोषी होगा। आपराधिक बल प्रयोग के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं –
(1) किसी व्यक्ति के प्रति साशय बल का प्रयोग किया गया हो। (2) इस प्रकार का बल प्रयोग उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया हो।
(3) ऐसा बल प्रयोग किसी अपराध कार्य के करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति के प्रति उसका उपयोग किया जाय उसको क्षति, भय या क्षोभ (खीझ) कारित करने के आशय से किया गया हो।
प्रश्न 47. आपराधिक मानव वध क्या है?
What is culpable Homicide?
उत्तर- आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide)- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के अनुसार, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य कर के मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव-वध का अपराध करता है।
प्रश्न 48 आपराधिक मानव-वध को कब हत्या नहीं माना जाता है? State when Culpable Homicide does not amount to Murder?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के द्वितीय खण्ड में पाँच अपवादित परिस्थितियाँ (Exceptional Circumstances) का उल्लेख किया गया है जिनके अन्तर्गत मानव वध को हत्या का अपराधी न मानकर सदोष मानव वध का अपराधी माना जाता है। इस प्रकार पाँच अपवादित परिस्थितियाँ हैं-प्रथम, गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन (Grave and sudden Provocation) है। द्वितीय, वैयक्तिक निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण (Exceeding Right of Private Defence)। तृतीय, किसी लोकसेवक द्वारा अपने अधिकार शक्ति का अतिक्रमण (Exceeding the Right by Public Servant)। चतुर्थ, परिस्थिति आकस्मिक लड़ाई (Sudden fight) की है। पंचम, परिस्थिति मृतक की सहमति से कारित होने वाली मृत्यु (Death Caused by Consent of the deceased) है।
प्रश्न 49. व्यपहरण। Kidnapping.
उत्तर- व्यपहरण (Kidnapping)-व्यपहरण (Kidnapping) का शाब्दिक अर्थ है उठाकर ले जाना। परन्तु भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत व्यपहरण को बालचोरी (Child Stealing) के अर्थ में लिया गया है। व्यपहरण मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 359 व्यपहरण (Kidnapping) के प्रकार बताती है। इस धारा के अनुसार व्यपहरण (Kidnapping) दो प्रकार का होता है –
(1) भारत की सीमा से बाहर व्यपहरण;
(2) विधिपूर्ण संरक्षकता (Legal guardianship) से व्यपहरण ।
(1) भारत की सीमा से बाहर व्यपहरण – धारा 360 भारत में से व्यपहरण (Kidnapping from India) से सम्बन्धित प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जब किसी व्यक्ति को, उसकी सहमति के बिना या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना, जो उसकी ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत (authorised) है, भारत की सीमाओं के बाहर ले जाया जाता है तो भारत से व्यपहरण का अपराध गठित हो जाता है। इस धारा के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाता है, यह आवश्यक नहीं कि वह बच्चा ही हो। वह व्यक्ति बच्चा, जवान, वृद्ध, स्त्री, पुरुष हो, अथवा वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी।
(2) विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण- जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को या यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली की या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
प्रश्न 50. हत्या एवं आपराधिक मानव-वध में क्या अन्तर है? What is the difference between Murder and Culpable Homicide?
उत्तर- आपराधिक मानव वध एवं हत्या में अन्तर – न्यायमूर्ति मेलविल द्वारा रेक्स बनाम गोविन्दा, (1876) आई० एल० आर० 1 बम्बई 342 नामक बाद में आपराधिक मानव वध तथा हत्या के मध्य जो स्पष्ट अन्तर स्थापित किया गया है वह आज भी न्यायालयों के लिए उस विषय पर पथ-प्रदर्शन करता है।
सदोष मानव-वध (धारा 299 )
(Culpable Homicide)
कोई आपराधिक मानव-वध तब करता है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु की गई है –
(क) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो;
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो;
(ग) इस ज्ञान से किया गया हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाना सम्भव हो ।
हत्या ( धारा 300 ) (Murder)
कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव-वध हत्या है जब कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो –
(क) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो;
(ख) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधकर्ता जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना सम्भावित है जिसको वह क्षति पहुँचाई गई है;
(ग) किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से कार्य किया गया हो और वंह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो, कार्य की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। या
(घ) इस ज्ञान के साथ कार्य किया गया हो कि वह कार्य आसन्न संकट से इतना परिपूर्ण है कि हर अधि सम्भाव्यता के अन्तर्गत उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाएगी या वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा कि जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भव है।
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि (क), (ख) तथा (ग) के तत्व आपराधिक मानव-वध तथा हत्या के समान हैं। परन्तु मुख्य अन्तर मृत्यु कारित होने की सम्भावना पर निर्भर है। यदि अभियुक्त यह मानता है कि उसके कृत्य से मृत्यु सामान्य परिस्थिति में सम्भाव्य है तो वह सदोष मानव-वध होगा परन्तु यदि अभियुक्त यह मानता है कि उसकेकृत्य से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है या उसकी प्रबल सम्भावना है तो वह हत्या के अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार सदोष मानव-वध तथा हत्या के अन्दर अभियुक्त को मृत्यु होने की सम्भावना थी, के ज्ञान पर है। यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से मृत्यु होने की निश्चितता अधिक है तो हत्या है तथा यदि वह सिर्फ सम्भाव्यता पर विश्वास करता है तो उसका अपराध सदोष मानव-वध होगा।
प्रश्न 51. गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन।
Grave and Sudden Provocation.
उत्तर- गम्भीर एवं अचानक प्रकोपन (Grave and Sudden Provocation)- धारा 300 के द्वितीय खण्ड में दिये गये अपवाद 1 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अचानक तथा गम्भीर प्रकोपन दिलाया जाता है तथा उसके कारण वह अन्य व्यक्ति अपना आत्म-संयम खो देता है तथा प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है या यदि कोई व्यक्ति भूल या दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति हत्या का दोषी नहीं माना जाता तथा उसे सदोष (आपराधिक) मानव-वध का दोषी माना जाता है, क्योंकि गम्भीर प्रकोपन के अन्तर्गत किया गया कार्य आशयपूर्ण कार्य की तुलना में कम गम्भीर माना जाता है।
के० एम० नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 604 नामक प्रसिद्ध बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि प्रकोपन अचानक तथा गम्भीर तभी माना जायेगा यदि निम्न शर्तें पूरी हो –
(1) अभियुक्त युक्तियुक्त परिस्थितियों (Reasonable circumstances) में अपना आत्म-संयम खो बैठा हो।
(2) प्रकोपन कारित करने वाले व्यक्ति ने संकेतों या शब्दों के माध्यम से कोई ऐसा कार्य किया हो जो प्रकोपन या गम्भीर उत्तेजना का कारण हो, अर्थात् अभियुक्त को प्रकोपन या गम्भीर उत्तेजना मृतक द्वारा ही दिलाई गई हो।
(3) वाद या मामले की परिस्थितियों में मृतक द्वारा किया गया कार्य या बोले गयेशब्द किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को प्रकोपन के लिए पर्याप्त कारण हो ।
(4) मृत्यु का कारण प्रकोपन ही हो, प्रकोपन के अतिरिक्त कोई कारण मृत्यु या हत्या का कारण न हो।
प्रश्न 52. दहेज मृत्यु को परिभाषित कीजिए।
Define Dowry death.
उत्तर- दहेज मृत्यु (Dowry death)– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 (ख) में दहेज-मृत्यु को परिभाषित किया गया है, यह धारा भारतीय दण्ड संहिता में सन् 1986 के संशोधन द्वारा जोड़ी गयी।
धारा 304 (ख) के अनुसार-“जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा हो जाती है और उसकी मृत्यु के पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी माँग के लिए या इसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जायेगा।
प्रश्न 53. बलात्संग की परिभाषा दीजिए।
Define Rape. उत्तर- बलात्संग (Rape)– बलात्संग स्त्री के विरुद्ध किया जाने वाला गम्भीरतम अपराध है। बलात्संग की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में दी गयी है। यह धारा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित की गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई पुरुष –
(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारितकिया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,या
(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जायेगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भाँति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –
(1) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध (2) स्त्री की सहमति के बिना; (3) ऐसी सहमति किसी उपहति, जबरन या भय दिखाकर प्राप्त की गयी हो; (4) उस स्त्री की सहमति यह विश्वास करके ली गयी है कि वह उसका पति है जबकि वह उसका पति नहीं है, (5) सहमति विकृत चित्तता या मत्तता की अवस्था में दी गयी हो, (6) स्त्री की सहमति या बिना सहमति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है; (7) जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।
प्रश्न 54 सामूहिक बलात्संग।
Gang rape.
उत्तर- सामूहिक बलात्संग (Gang rape)- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (घ) जिसे दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ा गया है, में सामूहिक बलात्संग को प्रावधानित किया गया है-जहाँ किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुमनि से भी दण्डनीय होगा। दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 376 (घ) के आगे धारा 376 (घक) एवं धारा 376 (घख) जोड़कर सामूहिक बलात्कार के लिए दण्ड को और स्पष्ट एवं कठोर किया गया है अब जहाँ 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग किया जाता है वहाँ आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा तथा धारा 376 (घख) के अनुसार जहाँ 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग किया जाता है वहाँ हर व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से अथवा मृत्यु से दण्डित किया जायेगा।
प्रश्न 55 अपहरण से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Abduction?
उत्तर- अपहरण (Abduction)– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 362 में अपहरण (Abduction) की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण (मिथ्याकथन या कपटपूर्ण) उपायों द्वारा किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह व्यक्ति अपहरण (Abduction) का अपराध करता है। अपहरण में कपट या छल का तत्व विद्यमान रहना आवश्यक है।
प्रश्न 56. व्यपहरण एवं अपहरण में क्या अन्तर है?
What is difference between kidnapping and Abduction?
उत्तर- व्यपहरण (Kidnapping) तथा अपहरण (Abduction) में अन्तर –
व्यपहरण (Kidnapping)
(1) व्यपहरण 16 वर्ष से कम आयु के बालक या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या किसी भी उम्र के विकृत-चित्त (पागल) व्यक्ति के सम्बन्ध में होता है।
(2) व्यपहरण में एक व्यक्ति उस व्यक्ति की संरक्षकता से पृथक् किया जाता है जो व्यपहरित व्यक्ति की संरक्षकता के लिए प्राधिकृत है।
(3) व्यपहरण में बल प्रयोग आवश्यक नहीं है। व्यपहरित व्यक्ति को बहला फुसलाकर या उसकी या उसके संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से परे ले जाने को उत्प्रेरित किया जाता है।
(4) व्यपहरण में यदि अवयस्क या पागल व्यक्ति का व्यपहरण किया गया है तो संरक्षक की सहमति के बिना होता है तथा व्यपहरित व्यक्ति की सहमति महत्वपूर्ण नहीं है।
अपहरण (Abduction)
(1) अपहरण में आयु सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है, यह किसी भी आयु के व्यक्ति के सम्बन्ध में हो सकता है।
(2) अपहरण में अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है। उसमें संरक्षकता कोई मापदण्ड नहीं है ।
(3) अपहरण में बल प्रयोग या कपटपूर्ण दुर्भावना आवश्यक तत्व है।
(4) अपहरण यदि अपहरित व्यक्ति की सहमति से होता है तो अपहरण का अपराध गठित नहीं होता।
प्रश्न 57. चोरी को परिभाषित करें। Define Theft.
उत्तर- चोरी (Theft) – जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति लेने के लिए हटाता है तब वह चोरी करता है ऐसा कहा जाएगा। चोरी की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 में दी गयी है। धारा 378 के अनुसार-जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।
जैसे-‘य’ की सम्मति के बिना ‘य’ के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से ‘य’ की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को ‘क’ काट डालता है। यहाँ ज्यों ही ‘क’ ने इस प्रकार लेने के लिये उस वृक्ष को पृथक् किया, उसने चोरी की।
प्रश्न 58 उद्दापन से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Extortion?
उत्तर- उद्घापन (Extortion)– उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 383 के अन्तर्गत दी गई है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय से आशयपूर्ण ढंग से डालता है तथा इस प्रकार भय में डाले गये उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई ऐसी वस्तु जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदान करने हेतु बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करता है तो यह कार्य उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) कहलाता है।
‘क’, ‘ख’ को यह धमकी देता है कि यदि उसने उसे 5,000 रुपया नहीं दिया तो वह ‘ख’ के बारे में मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देगा। ‘ख’ को ‘क’ अपने धन को इस प्रकार देने के लिए उत्प्रेरित करता है। ‘क’ ने उद्दापन किया है।
प्रश्न 59. चोरी व उद्दापन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। Distinguish between Theft and Extortion.
उत्तर- चोरी तथा उद्दापन दोनों में एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करता है। चोरी तथा उद्दापन दोनों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सम्पत्ति वंचित करने का आशय बेईमानीपूर्ण होता है।
चोरी (Theft) तथा उद्दापन (Extortion) में अन्तर –
चोरी (Theft)
(1) चोरी के अपराध में अभियुक्त एकव्यक्ति के कब्जे से एक सम्पत्ति ले जाता है।
(2) चोरी में विषय-वस्तु सिर्फ चल सम्पत्ति है।
(3) चोरी में अभियुक्त सम्पत्ति के स्वामी की जानकारी के बिना, उसकी सहमति के अभाव में प्राप्त करता है।
(4) चोरी में बल का तत्व विद्यमान नहीं रहता है।
उद्दापन (Extortion)
(1) उद्दापन में अभियुक्त या तो स्वयं को या अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति देने के लिए विवश करता है।
(2) उद्दापन में विषय-वस्तु चल या अचल दोनों हो सकती है।
(3) उद्दापन में अभियुक्त सम्पत्तिधारी को में भय दिखाकर सम्पत्ति देने को विवश या उत्प्रेरित करता है तथा वह सम्पत्ति भय के अन्तर्गत जानबूझकर प्रदान करता है।
(4) उद्दापन के अपराध का आवश्यक तत्व बल प्रयोग या भय है ।
प्रश्न 60.कब चोरी लूट है?
When theft is robbery ?
उत्तर- कब चोरी लूट है- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 यह बतलाती है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।
चोरी “लूट” है, यदि उस चोरी को करने के लिये, या उस चोरी के करने में, या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का. या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।
उदाहरण-‘क’, ‘य’ को दबोच लेता है, और ‘य’ के कपड़े में से ‘य’ का और आभूषण ‘य’ की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। यहाँ, ‘क’ ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छया ‘य’ का सदोष अवरोध कारित करता है। इसलिए ‘क’ ने लूट की है।
प्रश्न 61. कब उद्दापन लूट है?
When extortion is robbery?
उत्तर- कब उद्दापन लूट है? – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 का पैरा द्वितीय “उद्दापन कब लूट होता है” के बारे में बतलाता है –
‘उद्दापन ‘लूट’ है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डाल कर इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है।”
दृष्टान्त- ‘क’, ‘य’ को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और ‘य’ की थैली माँगता है। परिणामस्वरूप ‘य’ अपनी थैली दे देता है। यहाँ ‘क’ ने ‘य’ को तत्काल उपहति का भय दिखला कर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अतः ‘क’ ने लूट की है।
प्रश्न 62. ‘अपराध समाज का वास्तविक दर्पण है।” टिप्पणी कीजिए।
“Crime is real mirror of society”. Comment.
उत्तर– अपराध समाज का वास्तविक दर्पण होता है, अपराध की अवधारणा सदैव लोकमत पर आधारित होती है, विधि की अवज्ञा को अपराध माना जाता है परन्तु विधि की प्रत्येक अवज्ञा अपराध नहीं है क्योंकि संविदा विधि व पारिवारिक विधि का उल्लंघन तब तक अपराध नहीं है जब कि ऐसा उल्लंघन किसी विधि द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए। जबकि एक साधारण व्यक्ति के लिए अपराध वह कार्य है “जिसे समाज में लोग घोर निन्दा के योग्य समझते हैं।” अपराध, विधि द्वारा निषिद्ध भी है तथा समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी है।
जैसे- हत्या, लूट तथा चोरी इत्यादि।
“अपराध विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है।”
ब्लैकस्टोन के अनुसार, “निषिद्ध या समादेशित करने वाले सार्वजनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।
स्टीफेन के अनुसार, “सम्पूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है।”
पैटन के अनुसार, “अपराध के सामान्य लक्षण हैं राज्य द्वारा कार्यवाही को नियन्त्रित करना, दण्ड को क्षमा करना तथा दण्ड देना।”
बेन्थम के अनुसार, “अपराध वह है जिन्हें विधि द्वारा अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया गया है।”
इन विभिन्न परिभाषाओं से निम्न तत्व सामने आते हैं –
(1) एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। तथा जो दण्ड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है;
(2) ऐसे मानव के मन में एक दुराशय है;
(3) ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य;
(4) ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या सम्पूर्ण समाज को एक क्षति ।
अतः अपराध को राज्य ने समाज की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है, अपराध को समाज का वास्तविक दर्पण कहना उचित ही है जो कि समाज के वास्तविक चेहरे को दिखलाती है।
प्रश्न 63 लूट तथा डकैती में क्या अन्तर हैं?
What are differences in Robbery and Dacoity?
उत्तर- लूट तथा डकैती (Robbery and Dacoity)-लूट तथा डकैती दोनों पर्यायवाची शब्द लगते हैं परन्तु विधिक रूप से लूट तथा डकैती में निम्न अन्तर हैं –
लूट (Robbery)
(1) लूट को धारा 390 में परिभाषित किया गया है।
(2) लूट में अभियुक्तों की संख्या पाँच से कम होती है।
(3) लूट का मामला डकैती का हो, यह आवश्यक नहीं है अर्थात् प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती।
(4) लूट में बल प्रयोग कम आवश्यक होता है।
(5) लूट के लिए दस वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।
डकैती(Dacoity )
(1) डकैती की परिभाषा धारा 391 में दी गई है।
(2) डकैती में अभियुक्तों की संख्या कम से-कम पाँच होनी आवश्यक है।
(3) डकैती का प्रत्येक मामला प्रथमदृष्ट्या लूट का होता है।
(4) डकैती में बल प्रयोग एक आवश्यक तत्व है।
(5) डकैती के लिए दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास या जुर्माना या आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है।
प्रश्न 64. डकैती को परिभाषित कीजिए।
Define Dacolty.
उत्तर- डकैती (Dacoity)- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 391 डकैती को परिभाषित करती है जिसके अनुसार, जबकि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में सहायता करते हैं, कुल मिलाकर पाँच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, वह ‘डकैती’ का अपराध करता है।
प्रश्न 65 सदोष परिरोध’ को परिभाषित कीजिए।
Define wrongful confinement.
उत्तर- सदोष परिरोध (Wrongful Confinement)- जब किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध इस प्रकार किया गया हो कि वह निश्चित परिसीमा से परे जाने से प्रतिबन्धित कर दिया गया हो तो उस व्यक्ति को इस प्रकार रोका जाना सदोष परिरोध कहा जाता है जैसा कि संहिता की धारा 340 में उपबन्धित है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का “सदोष परिरोध करता है। यह कहा जाता है।
सदोष परिरोध के निम्नलिखित दो आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं –
(i) अभियुक्त ने परिवादी का सदोष अवरोध किया हो, और
(ii) अभियुक्त ने परिवादी को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दिया हो।
प्रश्न 66 सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध में क्या अन्तर है?
What is the difference in Wrongful Restraint and Wrongful Confinement?
उत्तर- सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध में अन्तर- सदोष अवरोध की परिसीमा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 में दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी एक दिशा में जाने में बाधा उत्पन्न करता है तो वह सदोष अवरोध का अपराध करता है। जबकि सदोष परिरोध के अपराध में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी निश्चित सीमा से परे जाने से निवारित कर दे तो वह सदोष परिरोध का अपराध करता है।
प्रश्न 67. आपराधिक न्यास भंग।
Criminal Breach of Trust.
उत्तर – आपराधिक न्यास भंग – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405, आपराधिक न्यास-भंग (Criminal Breach of Trust) को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति पर कोई भी अधिकार, किसी प्रकार उसको न्यस्त किये जाने पर, उस सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है (Misappropriates dishonestly) या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार उस न्यास को संचालित करता है। या न्यास को संचालित करने वाला नियम या न्यास को संचालित करने के लिए किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा का अतिक्रमण करके सम्पत्ति का मनमानीपूर्ण ढंग से उपयोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित उक्त कार्यों को सहन करता है तो वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा।
प्रश्न 68 छल क्या है?
What is Cheating?
उत्तर- छल (Cheating)-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में छल (cheating) की परिभाषा दी गयी है। इस धारा के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रवंचना करके (झूठ बोलकर) प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित करता है या उस व्यक्ति को किसी सम्पत्ति को रखने हेतु, परिदत्त करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित करता है या यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित करता है कि वह उत्प्रेरित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे या किसी कार्य को करने में चूक करे जिससे उत्प्रेरित व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, ख्याति सम्बन्धी या सम्पत्ति से सम्बन्धित नुकसान हो तथा परिस्थितियाँ ऐसी हों कि कार्य या चूक करने वाला व्यक्ति प्रवंचना के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति ने छल किया है।
प्रश्न 69 प्रतिरूपण द्वारा छल।
Cheating by Personation.
उत्तर- प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by Personation)-भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित किया गया है। धारा 416 के अनुसार कोई व्यक्ति ” प्रतिरूपण द्वारा छल करता है” यह तब कहा जाता है, जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।
अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल करता है, तो वह धारा 416 के अन्तर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल करने का दोषी होता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया गया हो वह वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, वह काल्पनिक या कोई मृत व्यक्ति भी हो सकता है।
प्रश्न 70. लैंगिक उत्पीड़न से क्या अभिप्रेत है?
What is meant by sexual harassment?
उत्तर- लैंगिक उत्पीड़न (Sexual harassment) धारा 354 ( क ) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (क) को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न में ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात् –
(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक सम्बन्ध बनाने सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव अन्तर्वलित हों; या
(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई माँग या अनुरोध करने; या
(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने;
(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
ऐसा पुरुष जो खण्ड (i) या (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
जो पुरुष खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
प्रश्न 71. कब किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा।
When a man’s signature of his own name may amount to forgery?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 464 के स्पष्टीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में आ सकेगा। जैसे-‘क’ एक विनिमय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। ‘क’ ने कूटरचना की है।
प्रश्न 72. कूटरचना को परिभाषित कीजिए।
Define Forgery.
उत्तर- कूटरचना (Forgery)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 463 में ‘कूट रचना’ को परिभाषित किया गया है। धारा 463 के अनुसार, “जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रखता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाय, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति, सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट-रचना करता है।”
प्रश्न 73. मिथ्या साक्ष्य देने एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में क्या अन्तर है? Differenciate between false evidence and fabricating false evidence?
उत्तर- मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना में अन्तर –
(1) मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए अभियुक्त का केवल सामान्य आशय होना पर्याप्त है जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध में विशिष्ट आशय विद्यमान होना आवश्यक है।
(2) मिथ्या साक्ष्य देना किसी कार्यवाही की विशिष्ट तात्विक बात से सम्बन्धित होना आवश्यक नहीं है, परन्तु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध में मिथ्या गढे गये साक्ष्य का कार्यवाही के किसी तात्विक बात से सम्बन्धित होना आवश्यक है। जैसे ही मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, अपराध तुरन्त पूर्ण हो जाता है चाहे वह कार्यवाही के किसी बात से सम्बन्धित हो अथवा न हो।
(3) मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध के परिणामस्वरूप न्यायालय या लोक सेवक को कार्यवाही से सम्बन्धित किसी तात्विक बात के बारे में राय कायम करने में भ्रम या गलतफहमी उत्पन्न होना आवश्यक है, परन्तु धारा 191 के अन्तर्गत मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है।
(4) धारा 191 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी जाती है जो शपथ पर सत्य कहने के लिए आबद्ध है परन्तु धारा 192 के अपराध के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है।
(5) धारा 191 के अपराध के लिए जिस समय मिथ्या साक्ष्य दिया गया है उस समय कोई न्यायिक या गैर-न्यायिक कार्यवाही अस्तित्व में होनी चाहिए परन्तु धारा 192 के अपराध के लिए ऐसी कार्यवाही की भविष्य में सम्भावना होना मात्र पर्याप्त आधार होगा।
प्रश्न 74. छल एवं कूटरचना में क्या अन्तर है? What is difference in cheating and forgery?
उत्तर- छल तथा कूटरचना में अन्तर (Distinction between Cheating and Forgery)- छल तथा कूट-रचना (Forgery) दोनों में एक पक्षकार का आशय बेईमानीपूर्वक तथा कपटपूर्ण ढंग से अनुचित लाभ उठाना होता है। छल तथा कपट दोनों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कपटपूर्ण आचरण के कारण नुकसान या हानि उठाता है।
छल तथा कूटरचना में निम्न अन्तर हैं –
छल (Cheating)
(1) छल की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में दी गई है।
(2) छल के अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को असत्य कथन कर कोई कार्य या कार्यलोप करने को उत्प्रेरित करता है।
(3) छल के अन्तर्गत किसी को प्रवंचना, मिथ्या कथन के आधार पर सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है।
कूट-रचना (Forgery)
(1) कूटरचना (Forgery) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
(2) कूटरचना के अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेजों के भाग को रचता है।
(3) कूटरचना (Forgery) के अन्तर्गत मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज या दस्तावेजों के भाग के आधार पर किसी सम्पत्ति या हक पर दावा किया जाता है या दावे के समर्थन में उस कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न 75 रिष्टि क्या है? What is Mischief?
उत्तर- रिष्टि (Mischief)- रिष्टि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 में परिभाषित किया गया है। आशयपूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से हानि या नुकसान जनक कार्य करना रिष्टि (Mischief) है जिससे किसी सम्पत्ति का नाश हो या उस सम्पत्ति की स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि सम्पत्ति का मूल्य या सम्पत्ति की उपयोगिता कम होती हो या उस सम्पत्ति पर क्षति कारक प्रभाव पड़ता हो।
प्रश्न 76 आपराधिक अतिचार क्या है?
What is Criminal Trespass?
उत्तर- आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) (धारा 441 ) – सम्पत्ति के स्वत्व पर अन्यायपूर्ण अधिकार स्थापन को अतिचार की संज्ञा दी जा सकती है। भले ही यह अनधिकृत अधिकार स्थापन कितना ही अल्प क्यों न हो। परन्तु सभी अतिचार आपराधिक अतिचार नहीं हैं, सिर्फ वही अतिचार आपराधिक अतिचार होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अतिचार हों जिसका उस सम्पत्ति में कोई हित हो, जिस पर अतिचार किया गया हो।
आपराधिक अतिचार के निम्न आवश्यक तत्व हैं –
(1) किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर प्रवेश,
(2) यदि ऐसा प्रवेश वैध है तो वहाँ विधिविरुद्ध ढंग से उस सम्पत्ति पर बने रहना,
(3) उस सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर बने रहने का आशय,
(क) कोई अपराध करना हो,
(ख) कब्जाधारी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षोभ (खीझ) उत्पन्न करना हो ।
प्रश्न 77. द्विविवाह से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Bigamy?
उत्तर- द्विविवाह (Bigamy)-किसी विधिपूर्ण ढंग से विवाहित पुरुष या स्त्री द्वारा इस विधिपूर्ण विवाह के जारी रहते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह करना ही द्विविवाह है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 किसी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने अर्थात् द्विविवाह को प्रतिबन्धित करती है तथा द्विविवाह को एक दण्डनीय अपराध मानती है। यह धारा ऐसे द्वितीय विवाह को शून्य बनाती है। यह धारा सिर्फ हिन्दू, पारसी तथा ईसाइयों पर ही लागू होती है।
प्रश्न 78 बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Dishonest Misappropriation?
उत्तर – बेईमानीपूर्णदुर्विनियोग ( Dishonest Misappropriation ) – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग की परिभाषा देते हुए इस अपराध के लिए दण्ड निर्धारित करती है। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का, सम्पत्ति प्राप्त करते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था परन्तु सम्पत्ति प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पत्ति का बेईमानीपूर्ण आशय से सम्परिवर्तन कर लेता है तो वह व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोगः (Criminal Misappropriation) का अपराध करता है। अंग्रेजी विधि इसके प्रतिकूल है। अंग्रेजी विधि के अनुसार यदि सम्पत्ति प्राप्त करते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है परन्तु सम्पत्ति प्राप्त करने के पश्चात् वह उस सम्पत्ति का बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग कर लेता है तो । उसका ऐसा करना अपराध न होकर अपकृत्य होगा।
प्रश्न 79. मानहानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
What short notes on ‘Defamation.
उत्तर- मानहानि (Defamation)– भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 499 से 502 तक अपमान या मानहानि (Defamation) के अपराध से सम्बन्धित हैं। धारा 499 अपमान की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बोले गये शब्दों द्वारा या ऐसे लेखों द्वारा जिन्हें किसी द्वारा पढ़ा जाने का आशय हो, या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण करने द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई लांछन लगाता है तथा ऐसे लांछन से उस अन्य व्यक्ति की ख्याति (Reputation) को हानि होती है तो यह कहा जायेगा कि उसने उस अन्य व्यक्ति का अपमान किया है। यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करते हुए या यह विश्वास करने के कारण कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि उस लांछन से उस अन्य व्यक्ति की ख्याति अपहानि होगी तो भी यह कहा जायेगा कि उसने अपमान का अपराध किया है।
प्रश्न 80. “वक्रोक्ति” से आप क्या समझते हैं?
Write do you understand by “Innuendo”.
उत्तर- वक्रोक्ति (Innuendo)- वक्रोक्ति से तात्पर्य ऐसे कथन से है जो प्रथम दृष्ट्या मान हानिकारक कथन नहीं होता परन्तु उसका दूसरा अर्थ होता है, जो कि मानहानिकारक कथन साबित किया जा सकता है? अर्थात् कभी-कभी बोले गए या लिखे गये कथन प्रत्यक्षतः परिवादी को सम्बोधित नहीं किये गये होते, लेकिन परिवादी यह साबित करता है कि विशिष्ट परिस्थिति में वे उसके प्रति लांछनास्पद हैं और मानहानिकारक अर्थ रखते हैं। इसे वक्रोक्ति कहा गया, जो मानहानि का एक विशिष्ट रूप है। बी० सुबेर बनाम डॉ० पी० के० सुधाकरन, (1987) क्रि० लॉ ज० 736 (केरल) के वाद में अभियुक्त ने एक चिकित्सा व्यवसायी को उसका नाम लिए बिना व्यावसायिक व्यभिचारी तथा घटिया नैतिक चरित्र वाला कहा। परिवादी ने यह निःसन्देह रूप से साबित कर दिया कि अभियुक्त ने उक्त लांछनास्पद कथन उसी के प्रति किये थे, अतः अभियुक्त को धारा 499 के अन्तर्गत मानहानि के अपराध का दोषी ठहराया गया।
प्रश्न 81. गृहभेदन को परिभाषित कीजिए।
Define house breaking.
उत्तर- गृह भेदन (House Breaking)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 445 में गृह भेदन के बारे में उपबंध किया गया है। इस धारा का उद्देश्य आवासीय स्थलों की गोपनीयता को प्रतिरक्षित करना है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी आवासीय स्थल में अवैध रीति से प्रवेश करता है तो वह इस धारा के अन्तर्गत अधिक कठोर दण्ड से दण्डित होगा।
धारा 445 में गृह भेदन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –
जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है, वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह व्यक्ति उस गृह में या उस गृह के किसी भाग में इस धारा में वर्णित छः तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा उस गृह या उसके किसी भाग में अपराध के प्रयोजन से प्रवेश या अपराध कर चुकने पर, वर्जित प्रकारों से बाहर निकलता है, वर्णित छः प्रकार इस प्रकार हैं –
(1) यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए बनाया है,
(2) यदि अतिचारी ऐसे रास्ते से जो मानव प्रवेश के उद्देश्य से में बनाया गया हो, सीढ़ी या दीवार की सहायता से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।
(3) यदि अतिचारी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने तथा दुष्प्रेरक ने ऐसे साधन से गृह अतिचार के लिए खोला है, जिसका खोला जाना उस घर के स्वामी द्वारा आशयित नहीं था।
(4) यदि अतिचारी द्वारा गृह अतिचार करने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात् उस घर से निकलने के लिए किसी ताले को खोलता है। (5) यदि अतिचारी आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है,
(6) यदि अतिचारी किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बन्द किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है।
प्रश्न 82 आपराधिक अभित्रास।
Criminal intimidation.
उत्तर- आपराधिक अभित्रास (Criminal intimidation)-भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 503 में आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है। धारा 503 के अनुसार, “जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जायें, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिमार्जन करने के साधन स्स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभिनास करता है।”
प्रश्न 83. जारता । Adultery.
उत्तर- जारता (Adultery)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497 में जारकर्म को परिभाषित किया गया है। धारा 497 के अनुसार जारकर्म से तात्पर्य ऐसे संभोग से है जो किसी पुरुष द्वारा अन्य की पत्नी के साथ उस व्यक्ति की सम्पति के बिना अथवा उसकी मौन स्वीकृति के बिना किया जाता है। जिस महिला के साथ संभोग किया जाय वह किसी व्यक्ति की विधितः विवाहित पत्नी हो।
यदि कोई व्यक्ति (पुरुष) किसी अविवाहिता या विधवा या तलाकशुदा स्त्री के साथ संभोग करता है या उस स्त्री के पति की सम्मति या मौन स्वीकृति से उस स्त्री से संभोग करता है तो उसे जारकर्म के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा। धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म के अपराध का संज्ञान केवल विवाहिता महिला के पति की सम्मति या मौन स्वीकृति के बिना किसी पुरुष द्वारा उस महिला से संभोग किये जाने की दशा में ही लिया जा सकता है तथा इसलिए केवल पुरुष को ही दण्डित किया जा सकता है।
अतः इस धारा के अनुसार जारकर्म एक ऐसा अपराध है जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी पति के विरुद्ध उसकी पत्नी के प्रति किया जाता है।
डब्ल्यू० कल्याणी बनाम राज्य, ए० आई० आर० 2012 सु० को० 497 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की पत्नी को जारकर्म के दुष्प्रेरण का भी दोषी नहीं माना जा सकेगा क्योंकि महिला होने मात्र के आधार पर वह जारकर्म के अपराध से प्रतिरक्षित हो जाती है और उस अपराध के लिए उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस वाद में पत्नी द्वारा पति की गर्लफ्रेंड (जिससे अवैध लैंगिक सम्बन्ध हो) के विरुद्ध जारकर्म के दुष्प्रेरण का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया था।
प्रश्न 84. असम्भव प्रयास को स्पष्ट कीजिए।
Explain impossible attempt.
उत्तर- असम्भव प्रयास (Impossible Attempt)- पहले यह माना जाता था कि यदि एक व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है परन्तु अपराध कारित नहीं होता है तो वह व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। सामाग्री बनाम केलिन्स के बाद में एक व्यक्ति ने चोरी के आशय से एक व्यक्ति की जेब में डाला परन्तु जेब खाली होने के कारण वह चोरी करने में असमर्थ रहा अत: उसे चोरी के अपराध का दोषी नहीं माना गया। आर० बनाम डेविड (1868) के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का प्रयत्न करता है परन्तु वह असम्भाव्यता के कारण अपराध पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे दण्डित नहीं किया जा सकता। परन्तु उपरोक्त सिद्धांत को आर० बनाम रिंग, (1892) के बाद में पलट दिया गया। इस बाद में अभियुक्त को चोरी करने के आशय से एक महिला के हैण्डबैग में हाथ डालने के लिए दण्डित किया गया, भले ही उस हैण्डबैग में कुछ यहाँ मिला। अब आशय को महत्वपूर्ण माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि ‘अ’, ‘ब’ को भूलवश शक्कर को संखिया समझकर दूध में देता है तो वह हत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं होगा परन्तु यदि ‘अ’ ने ‘ब’ की हत्या करने के उद्देश्य से दूध में संखिया ही मिलाया हो परन्तु संखिया को अपर्याप्त मात्रा के कारण ‘ब’ न मरा हो तो ऐसी दशा ‘अ’ हत्या के प्रयत्न के अपराध का दोषी माना जायेगा।
प्रश्न 85. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 (A) में ‘निर्दयता’ को नवीन केस लॉ के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
Explain ‘Cruelty as contained in Section 498 (A) of L.P.C. with recent case law.
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498-क में किसी स्त्री पति द्वारा या पति के सगे सम्बन्धियों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता या जिसे सती का निवारण भी कहते हैं, का उपबंध किया गया है। यह धारा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा जोड़ी गई।
धारा 498 (क) के जोड़े जाने का प्रमुख उद्देश्य दहेज प्रताड़नाओं के मामले के निवारण हेतु समुचित दण्ड का प्रावधान करना था। यह धारा किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित करती है।
धारा 498 (क) में इस अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –
“वह व्यक्ति जो किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
स्पष्टीकरण- क्रूरता से तात्पर्य है कि –
(1) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है, या
(2) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई माँग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहा है।
पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 958 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्रूरता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह शारीरिक ही हो। मानसिक यातना भी इसके लिए पर्याप्त होती है। विवाह के दूसरे दिन से ही रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि लाने के लिए वधू को बार-बार ताने मारना, दुर्व्यवहार करना मानसिक यंत्रणा है।
प्रश्न 86 समस्यायें ।
Problems. समस्या 1. ‘क’ यह जानता है कि ‘य’ एक झाड़ी के पीछे है। ‘ख’ यह नहीं जानता। ‘य’ की मृत्यु करने के आशय से ‘ख’ को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ‘क’ उत्प्रेरित करता है। ‘ख’ गोली चलाता है और ‘य’ को मार डालता है। ‘क’ और ‘ख’ ने यदि कोई हो तो कौन से अपराध किये हैं? सकारण निर्णीत कीजिए।
‘A’ knows ‘Z’ to be behind a bush. ‘B’ does not know it. A. intending to cause ‘Z’s death, induced ‘B’ to fire at the bush. ‘B’ fires and kills ‘Z’. What offenses if any ‘A’ and ‘B’ have committed? Decide with reasons.
उत्तर- प्रस्तुत समस्या में ‘क’ हत्या का दोषी है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 के अनुसार, वह हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा। धारा 108 के अनुसार- दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध के करने में या किसी कार्य के करने में या किसी ऐसे कार्य के किये जाने में जो अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जैसा कि दुष्प्रेरक का है किया जाता तो अपराध होता, दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि आशय अथवा ज्ञान के अभाव में ‘ख’ चाहे हत्या के लिए दोषी हो या नहीं पर ‘क’ निश्चित रूप से हत्या का दोषी होगा।
समस्या 2. एक शिशु को ‘य’ के भोजन में विष डालने के लिए ‘क’ उकसाता है। और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल से ‘म’ के भोजन में, जो ‘य’ के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। क्या ‘क’ ने कोई अपराध किया है। सकारण उत्तर दीजिए।
A instigates a child to put poison into the food of ‘Z’ and gives him poison for the purpose. The child in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of ‘Y’ which is by the side of that of ‘Z’ Has ‘A’ committed any offence in the case? Answer giving reasons.
उत्तर- उपरोक्त समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 111 पर आधारित है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को एक कार्य हेतु दुष्प्रेरित करता है, परन्तु कोई भिन्न कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरक उसे किये गये कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी दायित्व के अधीन है, मानो उसने उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। इस धारा से जुड़ा दृष्टान्त (क) धारा को स्पष्ट करता है। दृष्टान्त (क) इस प्रकार है-एक शिशु को ‘य’ के भोजन में विष डालने के लिए ‘क’ उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल से ‘म’ के भोजन में जो ‘ब’ के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु ‘क’ के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है तो ‘क’ उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने शिशु को ‘म’ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो, दृष्टान्त ‘क’ के माध्यम से प्रश्नगत समस्या हल हो जाती है।
समस्या 3. ‘अ’ एक सर्जन, एक मरीज के पूछने पर उसे यह बता देता है कि वह बचेगा नहीं। वह मरीज इस सूचना से पहुंचे सदमें के कारण मर जाता है। ‘अ’ के अपराध की विवेचना कीजिए। ‘A’ a surgeon communicates to a Patient, when asked by him, tharhe can not survive. The Patient dies in consequence of the shock due to communication discuss liability of ‘A’. उत्तर- प्रस्तुत समस्या में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 93 के अनुसार ‘अ’ ने कोई अपराध नहीं किया है जो यह उपबन्धित करती है कि सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी जाती है, यदि उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो।
दण्ड संहिता में यह प्रावधान सम्भवतः इसलिए रखा गया है ताकि मरणासन्न व्यक्ति मरने के पूर्व अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले तथा वसीयत, दान, धर्म आदि को भी वह करना चाहता है उसे करके लौकिक कर्तव्यों तथा बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर सके।
समस्या 4. ‘ख’ को ‘य’ का गृह जलाने के लिए ‘क’ उकसाता है। ‘ख’ उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ सम्पत्ति की चोरी करता है। ‘क’ और ‘ख ने कौन से अपराध किये हैं? सकारण निर्णीत कीजिए।
‘A’ instigates ‘B to burn house. ‘B’ sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. What offences ‘A’ and ‘B’ have committed? Decide with reasons.
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 111 पर आधारित है जो धारा 111 के दृष्टान्त (ख) से मिलती-जुलती है। धारा 111 के अनुसार, “जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किये गये कार्य के लिए उसी प्रकार से तथा उसी विस्तार पर दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो।
परन्तुक – परन्तु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यन्त्र के अनुसरण में किया गया था, जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। अतः धारा 111 के निम्न आवश्यक तत्व हैं –
(i) कार्य जो किया गया, वह दुष्प्रेरण का सम्भाव्य परिणाम था और
(ii) वह दुष्प्रेरण संरचित करने वाले उत्प्रेरण अथवा सहायता के प्रभाव में या षड्यन्त्र के अनुसरण में किया गया था।
प्रस्तुत समस्या में ‘क’ द्वारा ‘ख’ को ‘य’ का मकान जलाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था, चोरी करने के लिए नहीं चोरी दुष्प्रेरण का सम्भाव्य परिणाम नहीं है। दूसरी बात चोरी सहायता अथवा षड्यन्त्र के अनुसरण में भी नहीं की गयी बल्कि ‘ख’ स्वयं अपने विचार से चोरी करता है।
अतः धारा 111 की जो दो उपरोक्त शर्तें हैं, उनके आधार पर ‘क’ मात्र गृह जलाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है जबकि ‘ख’ गृह जलाने के साथ ही साथ चोरी करने के अपराध का भी दोषी है।
समस्या 5. सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ‘ख’ को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ‘ख’ के घर जलाने की धमकी ‘क’ देता है। ‘क’ के आपराधिक दायित्व का निर्धारण कीजिए।
‘A’ for the purpose of induction ‘B’ to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B’s house. Determine the criminal liabilityof A.
उत्तर – प्रस्तुत समस्या में यहाँ ‘क’ आपराधिक अभित्रास का दोषी है। यह समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 पर आधारित है जो आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करती है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमको उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिमार्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभिवास करता है।”
अतः जहाँ सिविल बाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ‘ख’ को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ‘ख’ के घर को जलाने की धमकी ‘क’ द्वारा दी जाती है तो यहाँ ‘क’ धारा 503 के अन्तर्गत आपराधिक अभित्रास का दोषी होता है।
समस्या 6. ‘अ’ एक चाकू निकालकर ‘ब’ पर निशाना लगाकर ‘स’ से कहता है कि यदि वह सोने की जंजीर’अ’ को नहीं देती है तो वह उसके पुत्र ‘य’ की हत्या कर देगा। ‘अ’ ने कौन-सा अपराध किया है? कारण सहित उत्तर दीजिए।
‘A’ takes out a knife and aims it at ‘B’ and tells ‘C’ that he will kill her son ‘B’ if she does not give away the chain to ‘A’. What offence has ‘A’ committed? Give reasons for your answer.
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 390 से सम्बन्धित है जहाँ लूट को परिभाषित किया गया है। यहाँ प्रस्तुत समस्या में ‘अ’ लूट के अपराध का दोषी होगा क्योंकि यहाँ ‘अ’ ने ‘स’ को भय कारित करने के लिए वह उसके पुत्र ‘ब’ को तत्काल मृत्यु का भय दिखलाकर सोने को जंजीर पाना चाहता है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अत: ‘अ’ ने लूट की है।
समस्या 7. ‘रतन’ एक सन्दूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है किन्तु संदूक में कुछ नहीं मिलता है। ‘रतन ने कौन-सा अपराध किया है?
“Ratan’ makes an attempt to steel jewels by breaking a box but found nothing in it. What offence ‘Ratan’ has committed?
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 पर आधारित है जो अपराधों को करने के प्रयत्न से सम्बन्धित है चूँकि ‘रतन’ एक संदूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है भले ही संदूक में कुछ नहीं मिलता फिर भी उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है इसलिए वह चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा और वह इस धारा के अधीन दोषी मान जायेगा।
समस्या 8 ‘क’ को सदोष हानि करने के आशय से ‘क’ को मूल्यवान प्रतिभूति को ‘ख’ स्वेच्छया जला देता है। ‘ख’ के दायित्व का निर्धारण कीजिए।
‘B’ voluntarily burns a valuable security belonging to ‘A’ Intending to cause wrongful loss to ‘A’. Determine the liability of ‘B.
उत्तर- प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 के रिष्टि पर आधारित है। जो कोई इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे किसी सम्पत्ति का नाश या किसी सम्पत्ति में या उसको स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है।
यहाँ इस समस्या में ‘क’ की सदोष हानि कारित करने के आशय से ‘क’ की मूल्यवान प्रतिभूति को ‘ख’ स्वेच्छा से जला देता है। यहाँ ‘ख’ रिष्टि के अपराध का दोषी होगा।
समस्या 9. ‘अ’, ‘ब’ को ‘स’ की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। ‘ब’ ऐसा करने से इन्कार कर देता है। ‘स’ की कोई क्षति नहीं पहुंचती। क्या ‘अ’, ‘ब’ को ‘स’ को हत्या के लिए उत्प्रेरित करने का दोषी है?
‘A’ instigates ‘B’ to murder ‘C. ‘B’ refuse to do so. No harm is done to ‘C’. Is A guilty of abetting ‘B’ to murder C
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण (2) पर आधारित है –
स्पष्टीकरण ( 2 ) के अनुसार- दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाय या अपराध निर्मित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न हो।
चूँकि प्रस्तुत समस्या में ‘अ’, ‘ब’ को ‘स’ की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है और ‘ब’ ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ ‘अ’ हत्या करने के लिए ‘ब’ के दुष्प्रेरण का दोषी है।
समस्या 10. ‘रमेश’, एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में जो, ‘सुरेश के विरुद्ध पंकज के 1,000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि ‘सुरेश’ को ‘पंकज’ के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। क्या ‘रमेश’ ने मिथ्या साक्ष्य दिया?
Ramesh, in support of a just claim which Suresh has against Pankaj for one thousand rupees, falsely swears on a trial that he heard Suresh admit the justice of Pankaj’s claim has Ramesh Given false evidence.
उत्तर- हाँ, ‘रमेश’ ने मिथ्या साक्ष्य दिया। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में उपबन्ध किया गया है। धारा 191 के अनुसार-जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है और या तो, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। अतः ‘रमेश’ का कृत्य धारा 191 के तहत मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध है।
समस्या 11. ‘पप्पू’ एक बाक्स में, जो ‘माला’ का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बाक्स में पाये जायें और इस परिस्थिति में ‘माला’ चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाय, क्या ‘पप्पू’ ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है?
Pappu puts jewels in to a box belonging to Mala, with the intention that they may be found in that box and that this circumstance may cause Mala to be convicted of theft. Has Pappu fabricated false evidence?
उत्तर- हाँ, पप्पू ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा क्योंकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 192 में उपबन्ध किया गया है। धारा 192 के अनुसार जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, या मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज रखता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रवेष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक-सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति में मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कचन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिये तात्विक किसी बात के सम्बन्ध में गलत राय बनाये, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है” यह कहा जाता है।
समस्या 12. ‘क’ एक लोक ऑफिसर, न्यायालय के वारण्ट द्वारा ‘य’ को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ‘ख’ इस तथ्य को जानते हुये और यह भी जानते हुए कि ग, य नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग, य है और तद्द्द्वारा साशय क से ग को पकड़वाता है। ख के उत्तरदायित्व पर विचार-विमर्श करें।
A, a públic officer, B authorized by a warrant from a court of justice to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C, B not Z, willfully represent to ‘A’ that ‘C’ is Z and thereby intentionally causes ‘A’ to apprehend C. Decided ‘B’ responsibility.
उत्तर- प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 ‘किसी बात का दुष्प्रेरण’ पर आधारित है। इस धारा के अनुसार-वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। स्पष्टीकरण । के 1 अनुसार-जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है कि उसने दुष्प्रेरण किया ।
प्रस्तुत समस्या में क एक लोक सेवक है जो न्यायालय के वारण्ट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग य नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग. य है, और तद्द्द्वारा साशय क से ग को पकड़वाता है। यहाँ ख, ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।
समस्या 13. ‘विनोद’ एक भूधारक, यह जानते हुए कि उसकी भू-सम्पदा की सीमाओं के अन्दर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तिला देता है कि मृत्यु साँप काटने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से हुई है। ‘विनोद ने किस धारा के अन्तर्गत अपराध किया। स्पष्ट करें।
‘Binod”, a landholder, knowing of the commissions of a murder. within the limits of his estate, willfully misinforming the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. In which Section Committed offence by Binod? Explain.
उत्तर- ‘विनोद’ ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 177 के तहत मिथ्या सूचना देने का अपराध किया है। धारा 177 के अनुसार-जो कोई किसी लोक-सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा अतः विनोद, धारा 177 के तहत दण्डित किया जायेगा।
समस्या 14. ‘प्रवीण’ नामक व्यक्ति पुलिस वालों को यह गलत सूचना देता है कि महगाँव ग्राम के पास उस पर हमला किया गया है और उसे लूट लिया गया है। किन वह हमलावरों का नाम नहीं बताता किन्तु वह यह जानता है कि पुलिस इस सूचना के बाद उस गाँव की तलाशी लेगी जिससे ग्रामवासियों को क्षोभ होगा। ‘प्रवीण’ ने कौन सा अपराध किया? स्पष्ट करें।
Pravin falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighbourhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants, but knows it to be likely that in consequence of this information the police will make institute searches in the village to the annoyance of the villagers. Which offence committed by Pravin? Explain.
उत्तर- ‘प्रवीण’ ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 182 के तहत अपराध किया धारा 182 के अनुसार-जो कोई किसी लोक-सेवक को कोई ऐसी सूचना जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है इस आशय से देगा कि उस लोक सेवक को प्रेरित करे या यह सम्भाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको तद्द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक (क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे वह लोक-सेवक, यदि उसे उस सम्बन्ध में जिसके बारे में ऐसी इत्तिला दी गई है, तथ्यों को सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप करता, अथवा (ख) ऐसे लोक-सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
समस्या 15. ‘अ’ पत्र के माध्यम से ‘ब’ को ‘स’ की हत्या के लिए उकसाता है। ‘ब’ हत्या करने से इन्कार कर देता है। ‘य’ ने कौन-सा अपराध किया है ? यदि पत्र ‘ब’ के पास नहीं पहुँचता है तो ‘क’ द्वारा कौन-सा अपराध किया गया है?
उत्तर- उपरोक्त समस्या का प्रथम भाग भारतीय दण्ड संहिता की धारा 108 के दृष्टान्त (क) पर आधारित है, जिसके अनुसार ‘ग’ की हत्या करने के लिए ‘ख’ को ‘क’ उकसाता है। ‘ख’ वैसा करने से इन्कार कर देता है। ‘क’ हत्या करने के लिए ‘ख’ के दुष्प्रेरण का दोषी है। धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाय या अपराध गठित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। अतः यदि ‘ब’, ‘स’ की हत्या के लिए इन्कार कर देता है तो भी ‘क’ हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा तथा दण्डित किया जायेगा। फगुन काल बनाम असम राज्य, ए० आई० आर० 1959 सु० को० 673, इसी स्पष्टीकरण के अनुसार, ‘क’, ‘ख’ को दुष्प्रेरण हेतु पत्र प्रेषित करता है। पत्र ‘ख’ के पास नहीं पहुँचता तो ‘ख’ को पत्र की अन्तर्वस्तु का ज्ञान नहीं होता अतः ‘क’ दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होगा यदि पत्र की विषय-वस्तु का ज्ञान ‘ख’ को हो जाता है तो ‘क’ उत्प्रेरण के लिए दण्डित किया जायेगा। पत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण उस समय पूर्ण होता है जब पत्र की विषय-वस्तु निर्दिष्ट व्यक्ति की जानकारी में आ जाय। शिव दयाल बनाम सम्राट, (1894) 16 इलाहाबाद 339 परन्तु यदि पत्र निर्दिष्ट व्यक्ति तक नहीं पहुँचता तो वह यह केवल दुष्प्रेरण का प्रयत्न मात्र माना जायेगा। रेनसफोर्ड (1874) का मामला 13 कोम्स० १०
समस्या 16. ‘अ’ कार द्वारा इलाहाबाद से वाराणसी जा रहा था। ‘ब’ उसे रास्ते में मिलता है तथा उसे गोपीगंज तक ले जाने के लिए कहता है। ‘अ’ उसकी विनती को मान लेता है। परन्तु गोपीगंज पहुँचने के पश्चात् वह ‘ब’ को उतारता नहीं है तथा ‘ब’ के अनुनय-विनय के बावजूद वह उसे वाराणसी लाता है। ‘अ’ ने कौन-सा अपराध किया है?
उत्तर – उपरोक्त समस्या में ‘अ’ सदोष परिरोध का दोषी है। सदोष परिरोध की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 340 के अन्तर्गत दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार, यदि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा (घेर) से बाहर जाने से रोके (निवारित कर दे) तो वह सदोष परिरोध का दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या में ‘अ’ ने ‘ब’ को लिफ्ट दी। ‘ब’ को गोपीगंज ले जाया जाना था। ‘ब’ ने गोपीगंज उतार देने के लिए कहा। ‘अ’ ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा ‘ब’ को गोपीगंज नहीं उतारा अत: ‘ब’ को इसकी इच्छा के विरुद्ध वाराणसी तक जाना पड़ा। इस समस्या में ‘अ’ को ‘ब’ के सदोष परिरोध के लिए दोषी माना गया।
समस्या 17. एक महिला चिल्लाते हुए एक कुएँ की ओर दौड़ती है कि वह कुएँ में कूद जायेगी। परन्तु वह कुएँ के पास पहुँचे, उसके पूर्व उसे पकड़ लिया जाता है। क्या महिला ने कोई अपराध किया है?
उत्तर- उपरोक्त समस्या रमक्का बनाम सम्राट, (1884) 8 मद्रास 5 के वाद के तथ्य से मिली है। यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 से सम्बन्धित है जो अपराध के प्रत्यत्न को भी दण्डनीय अपराध मानती है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसे उस स्त्री की आत्महत्या की तैयारी मात्र कहा जायेगा क्योंकि कुएं में कूदने के आखिरी क्षण तक वह अपना विचार बदल सकती थी अतः उसे धारा 309 के अन्तर्गत आत्महत्या के प्रयत्न के लिए अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि आर० नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1994 एस० सी० 1844 में उच्चतम न्यायालय ने धारा 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था परन्तु बाद में हत्या के एक निर्णय द्वारा उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया तथा आत्महत्या के अपराध के बारे में स्थिति पूर्ववत् हो गई है।
समस्या 18. ‘ख’ पर ‘य’ आघात करता है। ‘ख’ को इस प्रकोपन से तीव्र कोष आ जाता है। ‘क’ जो निकट ही खड़ा हुआ है, ‘ख’ के क्रोध का लाभ उठाने और उससे ‘य’ का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ‘ख’ उस छुरी से ‘य’ का वध कर देता है। ‘क’ और ‘ख’ ने यदि कोई तो कौन से अपराध किये हैं? सकारण निर्णीत कीजिए।
‘Z’ strikes ‘B’, ‘B’ is by this provocation excited to violent rage. ‘A’ a bystander, intending to take advantage of ‘B’s hand for that purpose. ‘B’ kills ‘Z’ with the knife. What offences if any ‘A’ and ‘B’ have committed? Decide with reasons.
उत्तर- प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के आपवादिक दृष्टान्त से सम्बन्धित है। समस्या में चूँकि ‘क’, ‘ख’ के क्रोध को देखते हुए ‘य’ का वध करने का आशय रखता है। ‘ख’ के हाथ में एक दूरी थमाता है जिससे ‘ख’, ‘य’ की हत्या कर देता है। कार्य को आसान बनाने के दुष्प्रेरण के कारण यहाँ ‘क’ हत्या का दोषी है। जबकि यहाँ ‘ख’ चूँकि अचानक प्रकोपनवश ‘य’ की हत्या कर देता है इसलिए ‘ख’ आपराधिक मानव वध का दोषी है। [श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० (1975) एस० सी० 175]
समस्या 19. एक बैंक लूट में ‘अ’ और ‘ब’ बैंक में प्रवेश करते हैं, खजांची को गोली मार देते हैं और धन लेकर ‘स’ द्वारा चलाई गई एक कार से भाग जाते हैं जो बैंक के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। ‘द’ भी उनका सहयोगी है जो बाहर निगाह रखने के लिए नियुक्त है और यदि पुलिस आती है तो संकेत करे। जब पुलिस पहुँचती है तो ‘अ’ और ‘ब’ घटनास्थल से विलुप्त है और केवल ‘द’ गिरफ्तार किया जाता है। ‘द’ हत्या और लूट के लिए अभियोजित किया जाता है। विचारण के दौरान ‘द’ अभिकथन करता है कि उसने न तो बैंक में प्रवेश किया, न ही किसी का वध किया, न ही धन हुआ है और वह पूर्णतया निर्दोष है। ‘द’ के आपराधिक दायित्व का निर्धारण कीजिए।
At a bank robbery A and B entered in the bank, shot dead the cashier and took away the money in a car driven by C, who was waiting outside the bank. D was also their companion who was departed to keep a watch outside and give signal if the Police happened to arrive, By the time Police arrived A and B had vanished from the scene of occurrence and only D was arrested. D was prosecuted for murder and robbery. During the trial D said that he neither entered the bank nor killed anyone nor touched the money and he was quite innocent. Determine the criminal liability of D.
उत्तर – प्रस्तुत समस्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 पर आधारित है। धारा 34 के अनुसार-“जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है।” धारा 34 के निम्न आवश्यक तत्व हैं –
(1) एक आपराधिक कार्य किया गया हो।
(2) आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो।
(3) वह सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो।
प्रस्तुत समस्या में चूँकि ‘अ’ एवं ‘ब’ बैंक में प्रवेश करते हैं और खजाँची को गोली मार देते हैं ओर धन लेकर ड्राइवर ‘स’ के साथ कार से फरार हो जाते हैं ‘द’ जो कि उनका सहयोगी था जो बाहर निगाह रखा था कि यदि पुलिस आती है तो वह अपने साथियों को संकेत करे पुलिस के द्वारा केवल ‘द’ गिरफ्तार किया जाता है बाकी तीनों फरार हो जाते हैं ‘द’ को हत्या और लूट के लिए अभियोजित किया जाता है यहाँ ‘द’ भले ही न तो बैंक में प्रवेश किया और न ही किसी का वध किया और न ही धन हुआ है परन्तु वह अपने साथियों को सूचना देने के लिए खड़ा था अतः उसका कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया माना जायेगा। अतः धारा 34 में ‘द’ को आन्वयिक दायित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत दोषी माना जायेगा। अतः ‘द’ की दलील मान्य नहीं होगी।
वारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर, (1925) 52 आई० एल० आर० 197 के बाद में लार्ड समनर ने कहा है कि धारा 94 के अन्तर्गत घटना स्थल पर उपस्थिति ही पर्याप्त है।
अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ‘द’, ‘अ’ और ‘ब’ के साथ हत्या एवं लूट के लिए धारा 34 के अन्तर्गत आन्वयिक दायित्व के आधार पर दोषी होगा।