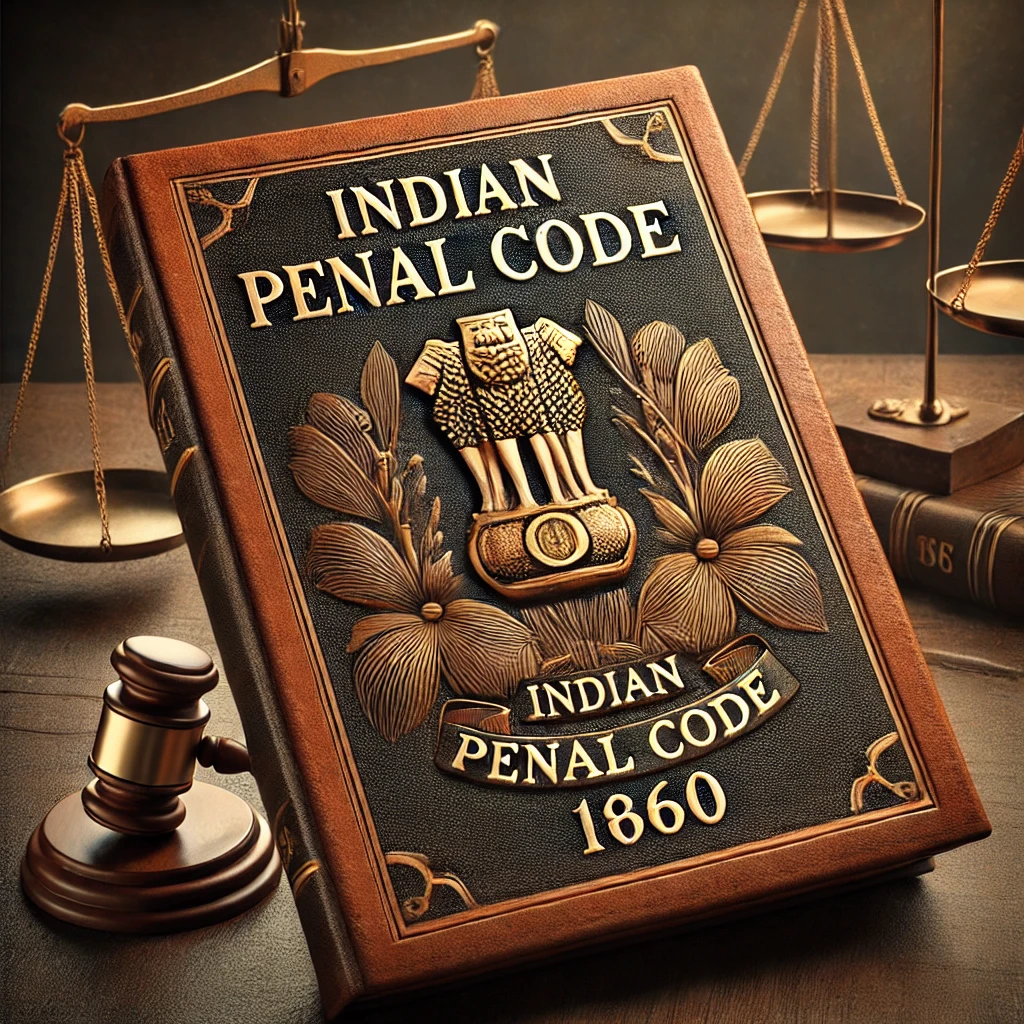– प्रथम सेमेस्टर –
प्रश्न 18 (ख) बलात्संग क्या है? बलात्संग के आवश्यक तत्वों की चर्चा करें तथा बलात्संग से सम्बन्धित विधि की भी चर्चा करें।
What is Rape? Discuss the essential elements of Rape and discuss the law relating to Rape?
उत्तर – बलात्संग (Rape ) – बलात्संग स्त्री के विरुद्ध किया जाने वाला गम्भीरतम अपराध है। बलात्संग की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में दी गयी है। इस धारा को दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई पुरुष –
(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या
(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,
तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भाँति को परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है –
(1) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध
(2) स्त्रो की सहमति के बिना
(3) ऐसी सहमति किसी उपहति, जबरन या भय दिखाकर प्राप्त की गयी हो
(4) उस स्त्री की सहमति यह विश्वास करके ली गयी है कि यह उसका पति है जबकि वह उसका पति नहीं है।
(5) सहमति विकृत चित्तता या मत्तता की अवस्था में दी गयी हो।
(6) स्त्री की सहमति या बिना सहमति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है।
(7) जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।
(1) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध – स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अर्थात् स्त्री की सहमति के विरुद्ध हो यहाँ यह आवश्यक है कि स्त्री ने यह जानते हुए कि उसके साथ क्या किया जाना है, अपनी सहमति दी हो। स्त्री का आपत्ति व्यक्त करने का ज्ञान हो या स्त्री अपनी सहमति व्यक्त करने में सक्षम हो यह ध्यान रहे कि इच्छा के विरुद्ध और सहमति के बिना दोनों समान नहीं है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई पुरुष किसी सोई हुई या मत्त या बेहोश स्त्री के साथ सम्भोग करता है तो वह जागने पर या होश में आने पर अपनी सहमति दे सकती है परन्तु उसके साथ किया गया सम्भोग उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध माना जायेगा। इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध शब्दावली सम्मति के विरुद्ध शब्दावली से अधिक विस्तृत है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री जादू-टोने या तथ्य की भूल के कारण सम्भोग हेतु सहमत हो जाती है तो यह नहीं कहा जाता कि सम्भोग के लिए उसकी इच्छा थी।
(2) सहमति के बिना – किसी भी स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ किया गया सम्भोग बलात्संग का अपराध माना जायेगा, सहमति सम्भोग कार्य से पूर्व होनी चाहिए उसके पश्चात् दी गयी सहमति का कोई महत्व नहीं है। आर० बनाम विलियम्स, (1923) के० बी० 340 नामक वाद में अभियुक्त एक संगीत शिक्षक था। उसने अपनी शिष्या के साथ यह कहकर सम्भोग किया कि इस कार्य से उसका सुर मधुर हो जायेगा। इस सहमति को कपटपूर्वक ढंग से प्राप्त सहमति मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को बलात्संग के अपराध का दोषी माना। एक व्यक्ति एक स्त्री से यह कहकर सम्भोग की सहमति प्राप्त करता है कि सम्भोग के पश्चात् वह उससे विवाह कर लेगा। यदि वह सम्भोग करने के पश्चात् विवाह करने से मुकर जाता है तो भी वह बलात्संग के अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सहमति धोखे से प्राप्त की गयी नहीं मानी जायेगी।
परन्तु किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, यदि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार पाण्डेय, ए० आई० आर० 2009 सु० को० 71 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि बलात्संग की शिकार स्त्री की आयु सोलह वर्ष से अधिक होने की स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा स्वयमेव यह उपधारणा की जाय कि स्त्री की उस दुष्कर्म में सहमति रही होगी, सरासर गलत एवं न्याय विरुद्ध है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में इस आधार पर अपील की गई थी कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का अभिलेख किये बिना ही प्रकरण में रेप की पीडित अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक होने के कारण उस दुष्कृत्य के लिए वह सम्मत थी, केवल यह उपधारणा करते हुए कि उक्त आयु के कारण उसकी सहमति रही होगी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, जो अनुचित एवं न्याय के विपरीत था। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने भी केवल इस उपधारणा के आधार पर तथा F.I.R. विलम्ब से दायर किये जाने को पर्याप्त कारण मानते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। राज्य द्वारा अपील में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त दोनों न्यायालयों के निर्णय को दोषपूर्ण एवं गलत मानते हुए उनके प्रति रोष व्यक्त किया तथा राज्य की अपील की स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और प्रकरण को उसे वापस पुनर्विचार हेतु प्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि वह इस पर कारणों सहित अपना निर्णय दें।
मुरुगन उर्फ सेत्तू बनाम तमिलनाडु राज्य, ए० आई० आर० 2011 सु० को० 1691 के बाद में अभियुक्त मुरुगन द्वारा एक 14 वर्षीय नाबालिग का व्यपहरण कर मन्दिर ले जाकर अपने दो सह अभियुक्तों की उपस्थिति में इससे जबरन विवाह कर लिया तथा उसके साथ अनेक बार बलात्संग किया। मुरुगन ने अपने बचाव में लड़की द्वारा लिखा प्रेम पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लड़की ने अपनी आयु 17 वर्ष दर्शाई थी और अभियुक्त से विवाह करने की आतुरता प्रकट की थी। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि बालिका जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र का स्कूल रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि से यह पूर्णत: साबित हो चुका था कि वह घटना के वक्त सिर्फ 14 वर्ष की थी। अतः अवयस्कता के कारण अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दण्डादेश दोनों ही उचित थे।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 बलात्संग के लिए दण्ड का उपबंध करती है कि जो कोई उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम को नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 376 के उपखण्ड (2) में पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लोक सेवक या लोक सेवक की अभिरक्षा में सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा या अस्पताल में या जेल, प्रतिप्रेषण गृह या हिंसा के दौरान या गर्भवती स्त्री से या स्त्री से बार-बार बलात्संग करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्रावृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। (दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित]
दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 376 में उपखण्ड (3) को अन्तःस्थापित किया गया है जिसके अनुसार, जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।
परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायेगा।
जो कोई धारा 376 की उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जायेगा तथा दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 376 (कख) जोड़कर 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग की दशा में कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास अर्थात् शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास और जुमनि से अथवा मृत्यु से दण्डित किया जायेगा।
प्रह्लाद सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1990 क्रि० लॉ ज० 1688 (राज०) के वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 376 के अपराध का विचारण केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः इस अपराध के आरोपी की मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है।
प्रश्न 19. चोरी की परिभाषा दीजिए। चोरी के आवश्यक तत्व क्या हैं? चोरी वउद्घापन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
Define Theft. What are essential ingredients of Theft? Distinguish between Theft and Extortion.
उत्तर– जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति लेने लिए हटाता है तब वह चोरी करता है, ऐसा कहा जायेगा। चोरी की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता धारा 378 में दी गयी है। धारा 378 के अनुसार- जो कोई किसी व्यक्ति कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।
स्पष्टीकरण 1– जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।
स्पष्टीकरण 2-हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है। चोरी हो सकेगी।
स्पष्टीकरण 3- कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है यह तब कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। स्पष्टीकरण 4- वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव-जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जोव-जन्तु को हटाता है और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गयी गति के परिणामस्वरूप उस जीव जन्तु द्वारा हटायो जाती है।
स्पष्टीकरण 5- परिभाषा में वर्णित सम्पत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। ‘य’ को सम्मति के बिना ‘य’ के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से ‘य’ की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को ‘क’ काट डालता है। यहाँ ज्योंही ‘क’ ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को भूमि से पृथक् किया उसने चोरी की।
जिस गृह पर ‘य’ का अधिभोग है उसमें मेज पर ‘य’ की अंगूठी ‘क’ को मिलती है। यहाँ वह अंगूठो ‘य’ के कब्जे में है, और यदि ‘क’ उसको बेईमानों से हटाता है, तो वह चोरी करता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से बिना उसकी सहमति लिये कोई जंगम सम्पत्ति हटाता है तो यह चोरी कहलायेगा। धारा 378 में दी गयी चोरी की परिभाषा को सरलता से समझने हेतु उसके आवश्यक तत्वों की चर्चा समीचीन होगी। चोरी के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं –
(1) अपराधी का सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय;
(2) चोरी के लिए सम्पत्ति जंगम होनी चाहिए,
(3) सम्पत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए;
(4) सम्पत्ति कब्जा रखने वाले व्यक्ति की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए;
(5) सम्पत्ति लेने के लिए सम्पत्ति को हटाया जाना चाहिए।
(1) बेईमानी से लेने का आशय – चोरी के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का होना चाहिए और यह बेईमानी का आशय सम्पत्ति को हटाने के समय ही होना चाहिए जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है-‘य’ के घर में मेज पर पड़ी हुई ‘य’ की अंगूठी ‘क’ देखता है। तलाशी तथा पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरन्त दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए ‘क’ उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका ‘य’ को कभी भी मिलना अति अनधिसम्भाव्य है इस आशय छपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे. यहाँ ‘क’ ने उस अंगूठी के प्रथम बार हटाते समय चोरी की है। तिलक राज कोहली बनाम राज्य, 1970 Cr.LJ 1961 दिल्ली के मामले में एक डाक लिपिक, जो पार्सल और अन्य डाक लेने का प्रभारी था, के विरुद्ध नकली रत्न के एक पार्सल को चुराने का आरोप था, यह धारित किया गया कि उसे चोरी के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्सल उसके कब्जे में वैध साधनों से आया था क्योंकि वह उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत था और उसका आशय बेईमानी से लेने का नहीं था। परन्तु यदि उसने बेईमानी से उसका दुर्विनियोग किया या उसे अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित किया, तो उसे आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है।
(2) कोई जंगम सम्पत्ति– चोरी केवल जंगम सम्पत्ति की ही होनी चाहिए। जंगम सम्पत्ति का अर्थ धारा 22 से लगाया जायेगा। इससे आशय यह है कि जंगम सम्पत्ति के अन्तर्गत हर भाँति को मूर्त सम्पत्ति आती है किन्तु भूमि व चीजें जो भू-सम्बद्ध हो या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इनके अन्तर्गत नहीं आतीं।
(3) किसी व्यक्ति के कब्जे में से – चोरी के अपराध के लिए आवश्यक है कि चोरी का सामान किसी के कब्जे में से हटाया गया हो। इस कब्जे की आवश्यकता के कारण जंगली पशुओं, पक्षियों और मछलियों, जब तक वे स्वतन्त्र हों, की चोरी सम्भव नहीं है। परन्तु पालतू पशुओं की चोरी सम्भव है। रामशरणागत बनाम राज्य, (1966) Cr.L.J. 856 पटना जहाँ एक सह-सम्पत्ति का सह- स्वामी, जिसके पास निश्चित भाग था, ने दूसरे सह-स्वामी के भाग को उसे सदोष हानि और स्वयं को सदोष अभिलाभ कारित करने के आशय से हटाया, वह चोरी के लिए दोषी ठहराया गया।
(4) उस व्यक्ति की सम्मति के बिना-चोरी के अपराध में सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की सम्मति के बिना सम्पत्ति ली जाती है। यह सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों हो सकती है और यह कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है। उदाहरणस्वरूप-‘य’ की सम्पत्ति को स्वयं अपनी होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ‘ख’ के कब्जे में से उस सम्पत्ति को ‘क’ ले लेता है। यहाँ ‘क’ बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता है। एक बाद में ‘ख’ के स्वामी को सम्पत्ति चुराने के लिए ‘क’ने ‘ख’ से सहयोग माँगा ‘ख’ ने सब कुछ अपने स्वामी को बतला दिया और फिर ‘क’ को चोरी के लिए दण्डित करवाने के लिए ‘ख’ ने चोरी में ‘क’ को सहायता की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ‘क’ चोरी के दुष्प्रेरण के लिए ही दोषी होगा, चोरी के लिए नहीं क्योंकि चोरी में सम्पत्ति कब्जा रखने वाले व्यक्ति की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए जबकि इस मामले में ‘ख’ के स्वामी को ‘क’ की योजना की जानकारी थी और स्वामी ने इस प्रकार ‘क’ को चोरी के लिए अपनी विवक्षित सम्मति दी थी ताकि वह और ‘ख’ मिलकर ‘क’ को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ सकें। [ टी० एन० चौधरी बनाम एम्परर (1878) 4 कलकत्ता 366]।
(5) सम्पत्ति लेने के लिए हटाता है – चोरी का अपराध तभी पूरा होता है जब अभियुक्त सम्पत्ति लेने के लिए हटाता है। चोरी के लिए सम्पत्ति का हटाया जाना आवश्यक है और हटाना सम्पत्ति लेने के लिए ही होना चाहिए अन्य किसी बात के लिए नहीं। कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति कैसे हटाई जाती है यह स्पष्टीकरण 1, 2, 3 स्पष्ट कर देता है। वेंकट स्वामी बनाम एम्परर, (1890) 14 229 के मामले में अभियुक्त जो डाकघर में कर्मचारी था, ने पत्रों की छंटाई करते समय दो पत्रों को इस आशय से निकाल लिया कि उन्हें स्वयं डाक बाँटने वाले व्यक्ति को देगा जिससे कि उन पर भुगतान किये जाने योग्य धन को वह और डाक बाँटने वाले व्यक्ति साझा रूप से प्राप्त कर सकें। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह चोरी के अपराध के लिए और आपराधिक दुर्विनियोग के प्रयत्न के लिए दोषी था।
चोरी व उद्दापन में अन्तर –
(1) चोरी की विषय-वस्तु सिर्फ चल सम्पत्ति होती है जबकि अपकर्षण या उद्यापन में विषय वस्तु चल या अचल दोनों हो सकती है।
(2) चोरी के अपराध में सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना सम्पत्ति प्राप्त की जाती है जबकि अपकर्षण या उद्दापन में स्वामी को भय के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है तथा सम्पत्ति का स्वामी इस सदोष सहमति के अन्तर्गत वस्तु या धन परिदत करता है।
(3) चोरी के अपराध में किसी भय या बल का प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि अपकर्षण के अपराध में सम्पत्ति के स्वामी को क्षति या उपहति पहुँचाने का भय उत्पन्न किया जाता है।
प्रश्न 20. (1) उद्दापन (अपकर्षण) के आवश्यक तत्वों की चर्चा करें क्या आपके विचार में ब्लैकमेल के प्रत्येक मामले उद्दापन भारतीय दण्ड संहिता में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं? Discuss the essential elements of Extortion. Do you think that every case of Blackmail is covered by definition of Extortion ndian Penal Code?
उत्तर- उद्घापन की परिभाषा – उद्दापन या अपकर्षण बलपूर्वक चोरी का एक उदाहरण है। जब किसी व्यक्ति को उसके अथवा किसी व्यक्ति के शरीर को क्षति कारित करने का भय दिखाकर उसकी सम्पत्ति से उसे वंचित किया जाता है तो उस कार्य को उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) कहते हैं।
उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 383 के अन्तर्गत दी गई है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में आशयपूर्ण ढंग से डालता है तथा इस प्रकार भय में डाले गये उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई ऐसी वस्तु जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदान करने हेतु बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करता है तो यह कार्य उद्दापन या अपकर्षण (Extortion) कहलाता है।
‘क’ ‘ख’ को यह धमकी देता है कि यदि उसने उसे 5,000 रुपये नहीं दिया तो वह ‘ख’ के बारे में मानहानिकारक अपलेख प्रकाशित कर देगा। ‘ख’ को ‘क’ अपने धन को इस प्रकार देने के लिए उत्प्रेरित करता है। ‘क’ ने उद्दापन किया है।
‘क’, ‘य’ को घोर क्षति कारित करने के भय में डालकर बेईमानीपूर्वक ‘य’ को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुहर (Seal) लगा दे और उसे ‘क’ को परिदत्त कर दे। ‘य’ उस कागज को हस्ताक्षर करके ‘क’ को परिदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए ‘क’ ने उद्दापन का अपराध किया है।
उद्दापन या अपकर्षण की आवश्यक शर्ते- धारा 383 के अन्तर्गत अपकर्षण या उद्दापन की दी गई परिभाषा के विश्लेषण से उद्दापन की निम्न आवश्यक शर्तें (तत्व) मिलती हैं –
(1) किसी व्यक्ति को चोट या गम्भीर क्षति के भय में डालना;
(2) स्वयं उस व्यक्ति को अथवा उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को भय दिया जाना;
(3) भय जानबूझकर दिया जाना,
(4) भयपूर्ण कार्य का आशय बेईमानीपूर्वक हो,
(5) ऐसे भय का उद्देश्य उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable securities) या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित वस्तु जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, परिदत्त करने के लिए भयग्रस्त व्यक्ति को उत्प्रेरित करना हो।
(1) किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालना – उद्घापन का प्रथम तथा प्रमुख तत्व यह है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भय में डालकर कोई वस्तु परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित करता है। यही तत्व उद्दापन को चोरी से पृथक् करता है। चोरों में गुप्त रूप से सम्पत्ति को स्वामी की जानकारी के बिना उसे सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। जबकि उद्दापन में एक व्यक्ति भय के प्रभाव में आकर भय कारित करने वाले व्यक्ति को स्वयं कोई वस्तु या धन परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित होता है। ऐसा भय शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित या किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित क्षति कारित करने का हो सकता है। जैसे मारने-पीटने की धमकी देना या परिरोध में रखने की (कैद में रखने की धमकी देना। अभियोग लगाने की धमकी देना या मानहानिजनक लेख प्रकाशित करने की धमकी देना। इसमें आध्यात्मिक दण्ड (Spiritual Punishment) की धमको सम्मिलित नहीं है। वह क्षति जिसका भय दिया गया है, अवैध होनी चाहिए। जैसे यदि एक पुरोहित विवाह के समय यह धमकी देता है कि यदि उसे 1,000 रुपया नहीं दिया गया तो वह विवाह कार्य पूर्ण नहीं करायेगा। उस धमकी को अपकर्षण या उद्दापन नहीं माना गया परन्तु यदि एक वकील अपने मुवक्किल को यह धमकी देता है कि यदि उसने उसे 100 रुपया नहीं दिया तो वह अभियोजन के साक्षियों से अपमानजनक, अप्रासंगिक तथा अभद्र प्रश्न पूछेगा, उसे अपकर्षण या उद्दापन माना गया।
(2) भय स्वयं उस व्यक्ति को या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का हो सकता है – यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह आवश्यक नहीं है कि भय उस व्यक्ति को क्षति कारित करने का हो जिसे सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है। यदि उत्प्रेरित होने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के लिए दिया जाता है तो भी भय देने वाला व्यक्ति उद्दापन (Extortion) का दोषी होगा। जैसे ‘क’, ‘ख’ से कहता है कि यदि ‘ख’ उसे 5,000 रुपया नहीं देता है तो वह उसके भाई को मारेगा या उसके पुत्र या उसके भतीजे को कैद में रखेगा। यदि इस धमकी के फलस्वरूप ‘ख’, ‘क’ को 5,000 रुपया देने को उत्प्रेरित होता है तो ‘क’ उद्घापन का दोषी होगा।
(3) भय जानबूझकर बेईमानीपूर्वक दिया जाना – उद्दापन के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति या अन्य प्रकार की क्षति का भय दिखाने का आशय बेईमानीपूर्वक कोई धन या कोई वस्तु परिदत्त करने हेतु प्रेरित करने का होना चाहिए। भय दिखाकर धन या वस्तु बेईमानीपूर्वक प्राप्त करने का आशय उद्दापन का महत्वपूर्ण तत्व है।
(4) उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security) किसी व्यक्ति को परिदत्त करना-उद्दापन का अन्तिम आवश्यक तत्व यह है कि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक अभिनास या मानहानि के भय से किसी अन्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत करने के लिए उत्प्रेरित होकर उसे परिदत कर है। जब तक सम्पत्ति के आधिपत्य का वास्तविक परिदान नहीं कर दिया जाता तब तक उद्घापन का अपराध गठित नहीं होता।
यह स्मरणीय है कि यदि एक व्यक्ति यह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उसकी कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास है तथा वह व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति से अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उस व्यक्ति को शारीरिक या अन्य प्रकार का भय दिखाता है तो वह उदापन का दोषी नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसका आशय बेईमानीपूर्वक वस्तु प्राप्त करना नहीं होता।
क्या ब्लैकमेल करने की धमकी से धन प्राप्त करना उद्दापन होगा?- धारा 383 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अपमानित करने या अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के भय के अन्तर्गत कोई धन परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है तो वह उद्दापन का अपराध होगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की धमकी देता है तो धमकीग्रस्त व्यक्ति अपमानित होने के भय से ही कोई वस्तु या धन परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित होता है। अतः ब्लैकमेल करने की धमकी के फलस्वरूप धन प्रदान करने हेतु उत्प्रेरित करना या धन प्राप्त करना उद्दापन का अपराध होगा।
प्रश्न 20. (ii) लूट क्या है? लूट के आवश्यक तत्व क्या हैं? कब एक लूट डकैती हो जाती है?
What is Robbery? What are essential ingredients of Robbery ? When does a Robbery become a Dacoity ?
उत्तर- लूट का अपराध चोरी या उद्दापन (Theft or Extortion) का ही एक गम्भीर रूप है, क्योंकि चोरी, उद्दापन तथा लूट तीनों में एक व्यक्ति का आशय दूसरे व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से उसे वंचित करना होता है। धारा 390 लूट के बारे में है परन्तु यह धारा लूट को परिभाषित करने के बजाय उसके स्थान पर उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें चोरी या उद्दापन लूट हो जाते हैं। इस प्रकार लूट, चोरी या उद्दापन का वह कृत्य है जो धारा 390 में वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत कारित होता है। अत: इस धारा के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।
चोरी कब लूट है?— चोरी “लूट” है, यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में, या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित का प्रयत्न करता है।
उद्दापन कब लूट है? – उद्दापन “लूट” है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में बालकर यह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहाँ ही परिदत करने के लिए उत्प्रेरित करता है।
लूट के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंसा के भय की मौजूदगी है। इस प्रकार लूट से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति से उसकी उपस्थिति में या उसकी इच्छा के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करके या उसे भय दिखलाकर उसके कब्जे से सम्पत्ति को प्राप्त करने से है।
लूट के अपराध के आवश्यक तत्व
(Essential Ingredients of Robbery)
(1) मृत्यु, उपहति या सदोष परिरोध का आसन भय (Imminent Danger of Death. Hurt or Wrongful Confinement) – जैसा कि पहले कहा गया है लूट, चोरी तथा उद्दापन का गम्भीर रूप है। इसलिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि लूट के अपराध में चोरी तथा उद्दापन के तत्व विद्यमान हैं। यदि चोरी या उद्दापन का अपराध करते समय या इस अपराध का प्रयत्न करते समय या चोरी या उद्दापन द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाते समय अभियुक्त क्षतिग्रस्त या व्यथित व्यक्ति को या तो उसके स्वयं के या अन्य व्यक्ति की मृत्यु, चोट या सदोष परिरोध का आसन्न या तत्काल भय दिखाता है तो अभियुक्त लूट के अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार यदि अभियुक्त पीछा किये जाने के कारण चोरी की सम्पत्ति वहीं छोड़कर भाग गया हो तथा पीछा करने वाले लोगों को डराने या धमकाने के लिए उन पर पत्थर फेंके हो तो उसे चोरी के प्रयास के लिए दण्डित किया जायेगा, लूट के अपराध के लिए नहीं।
इस प्रकार यदि ‘क’, ‘ख’ की सम्मति के बगैर, उसकी सम्पत्ति ले जाता है तथा ‘ख’ को यह भय दिखाता है कि यदि उसने प्रतिरोध किया तो उसे मार डाला जायेगा या उसके पुत्र या पत्नी को गम्भीर चोट पहुंचाई जायेगी तथा अपने भय को कार्यान्वित करने का आसन्न आशय प्रकट करता है तो ‘क’ लूट का दोषी होगा।
हरिशचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश (1976) नामक वाद में अभियुक्त ने चलती ट्रेन से एक व्यक्ति की घड़ी छीन ली। जब व्यक्ति व्यक्ति ने प्रतिरोध किया तो दूसरे अभियुक्त ने उसे थप्पड़ मारा न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोट चोरी से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित थी क्योंकि वह चोरी (घड़ी की चोरी) को सुगम बनाने के लिए पहुँचाई गई थी, अतः अभियुक्त को लूट के अपराध के लिए दण्डित किया जायेगा।
(2) चोरी या उद्दापन हेतु हिंसा या बल प्रयोग स्वेच्छा से किया गया हो – लूट का अपराध तभी घटित होगा यदि अभियुक्त द्वारा हिंसा या बल प्रयोग स्वेच्छया किया गया हो तथा उस हिसा या बल प्रयोग का आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या सदोष परिरोध करने का तात्कालिक भय (खतरा) उत्पन्न करना हो। यह भय या खतरा आसन्न (तत्काल) होना चाहिए न कि सम्भावित या कल्पित।
‘किसी व्यक्ति की सम्पत्ति’ पदावली में व्यक्ति शब्द की व्याख्या करते समय व्यक्ति में मृतक की देह सम्मिलित की जानी चाहिए। जमनादास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1963)
म० प्र० 106 नामक बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ‘व्यक्ति’ शब्द के अन्तर्गत मृत देह सम्मिलित है।
इस प्रकार यदि एक महिला के नाक से नथुनी खींचने के कारण महिला की नाक का ऊपरी भाग फट जाता है तो अभियुक्त लूट का दोषी होगा तथा यदि अभियुक्त ने महिला पर चाकू से अनेक वार किए तथा उससे सलवार के नारे से बाँधी चाबी को गुच्छी देने के लिए विवश किया तो अभियुक्त को लूट का दोषी मानकर दण्डित किया जायेगा।
यदि कई अभियुक्त लूट में शामिल हों तथा एक व्यक्ति अपराध को सुगम बनाने के लिए क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान के बाहर खड़ा होकर संकट की चेतावनी देने के लिए तैनात किया जाता है तो वह यह तर्क नहीं दे सकता कि उसने लूट में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था।
लूट कब डकैती हो जाती है?- जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं तो यह डकैती का अपराध हो जाता है। डकैती को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 391 में परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, जब कि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहाँ कि वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किये जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पाँच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह ‘डकैती’ करता है।
इस प्रकार लूट और डकैती में कोई विशेष अन्तर नहीं है सिवाय इसके कि लूट के मामले में अपराधियों की न्यूनतम संख्या निश्चित नहीं की गई है परन्तु डकैती में कम से कम पाँच व्यक्ति का संयुक्त रूप से शामिल होना आवश्यक है। रामलखन बनाम राज्य, ए० आई० आर० (1983) सु० को० 352 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि यदि पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध डकैती का अभियोग चलाया गया हो और उनमें से दो को सन्देह का लाभ देकर छोड़ दिया जाता है, तो शेष बचे तीन अभियुक्तों को डकैती के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।
हीरा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ए० आई० आर० (2007) सु० को० 2425 के वाद में पेट्रोल पम्प में हुई डकैती एवं लूट के अपराध में सात अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि की गई जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उचित ठहराते हुए अभियुक्तों की अपील निरस्त कर दी। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने पर न्यायालय ने दो अभियुक्तों को धारा 395 (भारतीय दण्ड संहिता) के अधीन की गई दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराते हुए अभिकथन किया। साक्ष्य तथा अभियुक्तों की पहचान परेड में की गई। शिनाख्त के आधार पर किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं थी। अन्य पाँच सह अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
लूट तथा डकैती में अन्तर- नूट तथा डकैती दोनों पर्यायवाची शब्द लगते हैं परन्तु विधिक रूप से लूट तथा डकैती म निम्न अन्तर हैं –
लूट (Robbery)
(1) लूट को धारा 390 में परिभाषित किया गया है।
(2) लूट में अभियुक्तों की संख्या पाँच से कम होती है।
(3) लूट का मामला डकैती का हो, यह आवश्यक नहीं है अर्थात् प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती।
(4) लूट में बल प्रयोग कम आवश्यक होता है।
(5) लूट के लिए दस वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।
डकैती (Dacoity)
(1) डकैती की परिभाषा धारा 391 में दी गई है।
(2) डकैती में अभियुक्तों की संख्या कम से कम पाँच होनी आवश्यक है।
(3) डकैती का प्रत्येक मामला प्रथमदृष्ट्या लूट का होता है।
(4) डकैती में बल प्रयोग एक आवश्यक – तत्व है ।
(5) डकैती के लिए दस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास या जुर्माना या आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान है।
प्रश्न 21. आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग क्या है? उपयुक्त दृष्टान्तों की सहायता से समझाइये। आपराधिक दुर्विनियोग किस प्रकार आपराधिक न्यास भंग से भिन्न है?
What is Criminal Misappropriation and Criminal Breach of Trust. Discuss with the help of suitable illustrations. How is criminal misappropriation different from criminal breach of trust?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा दी गई है तथा इसके लिए दण्ड भी निर्धारित किया गया है। धारा 403 के अनुसार, “यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी चल सम्पत्ति का दुर्विनियोग करेगा, या उस चल सम्पत्ति को अपने उपयोग में ले लेगा तो वह सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग (आपराधिक दुर्विनियोग) करता है इसके लिए उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।”
उदाहरण- हर्ष और हर्षित एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। हर्ष उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ‘हर्षित’ के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहाँ, हर्ष को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए यह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं है। किन्तु यदि ‘हर्ष’ उस घोड़े को बेच देता है, और सम्पूर्ण आगम (Sale) का अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।
स्पष्टीकरण 1- धारा 403 के अन्तर्गत दुर्विनियोग में अस्थायी तथा स्थायी दोनों ही प्रकार के दुर्विनियोग आते हैं।
स्पष्टीकरण 2- यह स्पष्टीकरण इस तथ्य को सुस्पष्ट करता है कि कोई परित्यक्त वस्तु दुर्विनियोग की विषय-वस्तु नहीं हो सकती।
आपराधिक दुर्विनियोग के आवश्यक तत्व-धारा 403 के अन्तर्गत अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: –
(1) बेईमानीपूर्वक सम्पत्ति का दुर्बिनियोग या स्वयं के उपयोग के लिए सपरिवर्तन,
(2) चल सम्पत्ति हो:
(3) प्रश्नगत सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी हो
(1) बेईमानीपूर्वक सम्पत्ति का दुर्विनियोग या स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तन – धारा 403 के अन्तर्गत आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भ में बेईमानी का कोई आशय न रहा हो। परन्तु बाद में उसके आशय में परिवर्तन के कारण या किसी नये तथ्य की जानकारी के परिणामस्वरूप अभियुक्त ने उस सम्पत्ति को सदोष या कपटपूर्वक अपने पास बनाये रखा हो। दुर्गा प्रसाद खोसला बनाम आर० ए० रहमानी, (1965) 2 इलाहाबाद 82 के मामले में यह कहा गया है कि धारा 403 के अन्तर्गत परिभाषित अपराध के लिए अभियुक्त को आपराधिक मन:स्थिति महत्वपूर्ण तत्व है न कि दुर्विनियोजित की गई वस्तविक धनराशि।
(2) चल सम्पत्ति हो – धारा 403 के अन्तर्गत अपराध की विषय-वस्तु केवल चल सम्पत्ति हो हो सकती है।
फूलचन्द्र दुबे बनाम सम्राट, (1929) 52 इलाहाबाद 200 के बाद में कहा गया है कि किसी भटके हुए बैल को कब्जे में लेकर बाँध रखना तथा उपयोग में लाना सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग माना गया।
(3) प्रश्नगत सम्पत्ति का कोई अन्य स्वामी होना आवश्यक है- धारा 403 के अधीन आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल तभी गठित हो सकेगा जब दुर्विनियोग या सम्परिवर्तन की गई सम्पत्ति का कोई अन्य व्यक्ति (अभियुक्त को छोड़कर) वास्तविक स्वामी हो। यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में कोई सम्पत्ति मिलती है और उसे उस सम्पत्ति के स्वामी के बारे में जानकारी होते हुए भी वह उसे लौटाने के बजाय स्वयं के उपयोग में लाता है, तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। परन्तु यदि उसे वास्तविक स्वामी का पता नहीं लगा है, तो वह इस अपराध का दोषी नहीं होगा और साथ ही साथ उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह युक्तियुक्त खोजबीन करके उस वस्तु के वास्तविक स्वामी का पता लगाए और उसे वह वस्तु वापस लौटा दे।
आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust) – जब किसी सम्पत्ति को लोक कल्याण या धर्मार्थ कार्यों के लिए सौंपा जाता है तो ऐसा उस सम्पत्ति का न्यास सृजित करके किया जाता है। इस न्यास की व्यवस्था तथा समयक् संचालन हेतु कुछ व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती है जिसे न्यास-मण्डल कहा जाता है। इस न्यास मण्डल का अध्यक्ष न्यासी (Trustee) होता है। न्यासी-न्यास की सम्पत्ति का संरक्षक माना जाता है। उसका विधिक तथा नैतिक कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यास की सम्पत्ति का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाय जिसके हेतु न्यास सृजित किया गया है तथा न्यास जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए सृजित किया गया है, उन्हें न्यास की सम्पत्ति का लाभ प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, न्यासी का यह कर्तव्य है कि वह न्यास की सम्पत्ति का उपयोग स्वयं के हित के लिए न करे तथा न्यास की सम्पत्ति की सम्यक् व्यवस्था सुनिश्चित कर उसके दुरुपयोग को रोके, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह न्यास-भंग का दोषी होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405, आपराधिक न्यास-भंग (Criminal Breach of Trust) को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति पर कोई भी अधिकार, किसी प्रकार उसको न्यस्त किये जाने पर, उस सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है (Misappropriates dishonestly) या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार उस न्यास को संचालित करता है या न्यास को संचालित करने वाला नियम या न्यास को संचालित करने के लिए किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा का अतिक्रमण करके सम्पत्ति का बेईमानीपूर्ण ढंग से उपयोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित उक्त कार्यों को सहन करता है तो वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा।
आपराधिक न्यास-भंग के आवश्यक तत्व (Essential Ingredients of Criminal Breach of Trust) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 के अन्तर्गत आपराधिक न्यास-भंग का अपराध गठित होने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है –
(1) अभियुक्त को सम्पत्ति के न्यासी के रूप में सम्पत्ति का स्वाभित्व सौंपा गया हो।
(2) अभियुक्त ने ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से
(i) दुर्विनियोग किया हो;
(ii) अपने स्वयं के उपयोग हेतु उसका संपरिवर्तन किया हो;
(iii) उसका उपयोग तथा व्ययन किया हो।
(3) उसने या उसकी उत्प्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने उस न्यास को नियन्त्रित करने वाली विधि के निर्देश का अतिक्रमण किया हो या उससे सम्बन्धित किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा का उल्लंघन किया हो।
(1) अभियुक्त को सम्पत्ति का स्वामित्व सौंपा जाना- न्यास के अन्तर्गत सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्पत्ति न्यासी को इस विश्वास के साथ सौंपी जाती है कि जिस व्यक्ति को सम्पत्ति सौंपी जा रही है वह सम्पत्ति का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेगा जिन उद्देश्यों के लिए सम्पत्ति उसे सौंपी गई है। लेक बनाम सिमन्स, (1927) ए० सी० 487 नामक वाद में न्यायमूर्ति हेल्डेन ने विचार व्यक्त किया कि यदि किसी व्यक्ति को धोखा देकर सम्पति सौंपने हेतु प्रेरित किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पत्ति न्यास के अन्तर्गत विश्वासपूर्वक सौंपी गई है।
एक वाद में एक स्त्री ने टिकट खिड़की पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण टिकट खिड़की के पास खड़े अभियुक्त को उसके लिए टिकट खरीदने के लिए बीस रुपये दिये, उस व्यक्ति ने उक्त महिला से वह रकम ले ली परन्तु उसे टिकट खरीदकर देने के बदले वह रुपये लेकर वहाँ से भाग गया। अभियुक्त न्यास-भंग के लिए दोषी है।
(2) बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग (Dishonest Misappropriation)– आपराधिक न्यास भंग के लिए सौंपी गई सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग आवश्यक है। कौशल्या बनाम राज्य, (1968) नामक बाद में एक स्त्री ने अभियुक्त के पास आभूषण गिरवी रखा परन्तु वह उसका उपयोग कर रहा था। स्त्री ने आभूषण की वापसी पर ब्याज देने से इन्कार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त ने स्त्री से आभूषण वापस ले लिए। न्यायालय के अनुसार, यहाँ अभियुक्त का आशय बेईमानीपूर्ण न होने के कारण वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी नहीं है।
मधुसूदन मेहरोत्रा बनाम किशोर चन्द भण्डारी, (1988) नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी के आभूषण पति के पास न्यासवत् रहते हैं तथा विवाह विच्छेद के पश्चात् पति उसे पत्नी को लौटाने के लिए बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा तथा परिवीक्षा के लिए अवधि गणना उस तिथि से होगी जब पति ने आभूषण लौटाने से अन्तिम बार इन्कार किया।
मोहन बनाम राजस्थान राज्य, (1960) में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि एक शराब-विक्रेता शराब बिक्री के लिए किसी को नौकर रखता है तथा उनके मध्य यह संविदा है कि नौकर बिक्री के एक निश्चित अंश को पारिश्रमिक के रूप में रख सकता है तथा नौकर यदि शराब में पानी मिलाकर अपने पारिश्रमिक में वृद्धि करता है तो वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा।
(3) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की उत्प्रेरणा से आपराधिक न्यास भंग किया जाना- यदि कोई व्यक्ति स्वयं न्यास भंग न करके किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक न्यास भंग के लिए उत्प्रेरित करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यास-भंग किया जाना सहन करता है तो भी वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा। इस प्रकार यदि कुछ व्यक्ति पानी का उपयोग नगर निगम की अनुमति के बिना करते हैं तथा नगर निगम का निरीक्षक उसकी सूचना नगर निगम को नहीं देता हो तो वह आपराधिक न्यास-भंग का दोषी होगा।
आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास-भंग में अन्तर– किसी अन्य व्यक्ति की चल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार प्राप्त कर उसका बेईमानीपूर्ण ढंग से स्वयं के स्वार्थ के लिए उपयोग करना आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, जबकि सद्भावपूर्वक किसी अन्य की अचल या चल सम्पत्ति से युक्त होने पर उसका अपने हित के लिए उपयोग आपराधिक न्यास-भंग का अपराध है। आपराधिक दुर्बिनियोग धारा 403 में परिभाषित किया गया है तथा आपराधिक न्यास-भंग धारा 405 में परिभाषित किया गया है। दोनों में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक स्वयं के हित के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों में बेईमानीपूर्वक आशय (dishonest intention) का तत्व आवश्यक है।
बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग में अन्तर –
बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग
(1) बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग को धारा 403 में परिभाषित किया गया है।
(2) बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग में सम्पत्ति का कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।
(3) बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग में पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार के करारगत (contractual) सम्बन्ध नहीं होते।
(4) बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग में सम्पत्ति किसी को सौंपी नहीं जाती, आ जाती है।
(5) बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग चल सम्पत्ति से ही सम्बन्धित है।
आपराधिक न्यास-भंग
(1) आपराधिक न्यास-भंग के अपराध को धारा 405 में परिभाषित किया गया है।
(2) आपराधिक न्यासभंग में सम्पत्ति का आधिपत्य विधिपूर्ण रीति से न्यास के रूप में प्राप्त किया जाता है।
(3) आपराधिक न्यासभंग में पक्षकारों के मध्य करारगत (contractual) सम्बन्ध होते हैं।
(4) आपराधिक न्यासभंग में एक व्यक्ति को विश्वासपूर्ण आशय के अन्तर्गत सम्पत्ति सौंपी जाती है तथा अभियुक्त उस विश्वास को भंग करता है।
(5) आपराधिक न्यासभंग चल या अचल किसी भी सम्पत्ति से सम्बन्धित हो सकता है।
प्रश्न 22. (1) छल को परिभाषित कीजिए। छल के आवश्यक तत्वों की चर्चा करें। छल कूटरचना से किस प्रकार भिन्न है?
Define cheating. Discuss the essential of cheating. How cheating differs from that of Forgery?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 छल (Cheating) की परिभाषा देती है। इस धारा के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रवंचना करके (झूठ बोलकर) इस प्रबंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित करता है या उस व्यक्ति (प्रवंचना करने वाले) को किसी सम्पत्ति को रखने हेतु परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित करता है कि वह उत्प्रेरित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे या किसी कार्य को करने में चूक (Omission) करे जिससे उत्प्रेरित व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, ख्याति सम्बन्धी (Relating to Reputation) या सम्पत्ति से सबन्धित नुकसान हो तथा परिस्थितियाँ ऐसी हो कि कार्य या चूक करने वाला व्यक्ति प्रवंचना के अभाव में नुकसानदायक कार्य या चूक (लोप) न करता तो यह कहा जायेगा कि प्रवंचना के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति ने छल (Cheating) किया है।
“क’ आशयपूर्ण ढंग से प्रवंचना करके ‘य’ को यह विश्वास दिलाता है कि ‘क’ ने ‘य’ के साथ की गयी संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है जबकि वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया है और एतद्वारा ‘य’ को बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करता है कि ‘य’, ‘क’ को वह धन दे। ‘क’ने ‘य’ से छल किया है।
‘क’, ‘ख’ को एक सम्पत्ति बेचता है। ‘क’ यह जानते हुए कि विक्रय की सम्पत्ति पर उसे कोई अधिकार नहीं है। ‘क’, ‘ख’ को किए गए विक्रय को छुपाते हुए वही सम्पत्ति ‘च’ को बेचता है या बन्धक रखता है तथा ‘च’ से विक्रय-धन या बन्धक धन प्राप्त कर लेता है तो यह कहा जायेगा कि उसने छल किया है।
इस प्रकार यदि एक व्यक्ति, आशयपूर्ण ढंग से तथा बेईमानीपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को असत्य कथन करके कोई सम्पत्ति परिदत करने हेतु या कोई ऐसा कार्य या चूक करने के लिए प्रेरित करता है जिससे उस व्यक्ति को कोई शारीरिक या अन्य प्रकार का नुकसान उठाना पड़े तो यह कहा जायेगा कि असत्य कथन करने वाले व्यक्ति ने छल किया है।
धारा 415 में दी गई छल की परिभाषा को सरलता से समझने हेतु उसके आवश्यक तत्वों को समझना होगा ये आवश्यक तत्त्व निम्न हैं: –
(1) किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को धोखा दिया हो अर्थात् एक तथ्य असत्य है, यह जानते हुए उस कथन को सत्य के रूप में बेईमानीपूर्वक अभिकथित किया हो।
(2) (क) वह कथन इस प्रकार कपटपूर्वक तथा बेईमानीपूर्वक किया गया हो जिससे –
(i) कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सम्पत्ति प्रदान करने हेतु प्रेरित हुआ हो:
(ii) किसौ सम्पत्ति को अपने पास रखने हेतु उत्प्रेरित हुआ हो,
(ख) जिस व्यक्ति को कपटपूर्ण कथन किया गया है वह कोई ऐसा कार्य करने या कार्यलोप करने के लिए प्रेरित (Induced) हुआ हो जिसे यदि इस प्रकार धोखा न दिया जाता तो वह न करता।
(3) उक्त कार्य या कार्यलोप (चूक) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को जिसे उत्प्रेरित किया गया है, कोई शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धित या सम्पत्ति सम्बन्धित हानि या नुकसान हुआ हो या होने की सम्भावना हो।
विभिन्न वादों के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया कि बेईमानीपूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र, परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, लाइसेन्स या पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु कपटपूर्वक उत्प्रेरित करना सम्पत्ति प्राप्ति हेतु उत्प्रेरित करना है।
यदि कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक कोई ऐसा कार्य करने या चूक करने के लिए किसी को उत्प्रेरित किया जाता है तथा जिस कार्य से जिसे उत्प्रेरित किया गया है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है तो उसे छल करना कहते हैं। सुशील कुमार दत्त बनाम राज्य (1985) नामक बाद में एक सवर्ण व्यक्ति ने स्वयं को अनुसूचित बताते हुए असत्य कथन किया तथा उसके आधार पर प्रशासनिक सेवा में चयनित होने में सफलता प्राप्त की, उसे छल के अपराध के लिए धारा 429 के अन्तर्गत दण्डित किया गया क्योंकि छल के लिए दण्ड का प्रावधान धारा 429 में है।
इस धारा के अन्तर्गत प्रवंचना या असत्य कथन कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक किया गया हो न कि सद्भावपूर्वक (With Good Faith)। उस तत्व के अन्तर्गत प्रवंचना या मिथ्या कथन करने वाले व्यक्ति का आशय एक प्रमुख तत्व होता है।
चिन्तामणि बनाम थानेश्वर (1974) नामक वाद में एक व्यक्ति ने सम्पत्ति क्रय करने से पूर्व विक्रेता से पूछा कि क्या सम्पत्ति सभी भारों से मुक्त है। इस पर विक्रेता ने बताया कि सम्पत्ति सभी भारों से मुक्त है परन्तु विक्रय के पश्चात् यह पाया गया कि सम्पत्ति भारों से युक्त थी। यह निर्णय दिया गया कि विक्रेता धारा 415 के अन्तर्गत छल का दोषी है।
यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि दूध में पानी मिला हुआ है, इस आशय से उस दूध को खरीदता है कि जिससे वह उस मिलावटी दूध बेचने वाले को पकड़वा दे, तो दूध बेचने वाले व्यक्ति को छल के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकेगा बल्कि वह छल के प्रयास के लिए अपराध का दोषी होगा।
हरी माँझी बनाम राज्य, (1990) नामक बाद में अभियुक्त ने एक लड़की के माता पिता को यह वचन दिया कि वह उससे विवाह करेगा। इसके पश्चात् वह लड़की से एक वर्ष तक शारीरिक सम्बन्ध बनाये रहा। इसके फलस्वरूप लड़की गर्भवती हो गई। उसे छल के लिए दोषमुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह साबित नहीं हो सका कि उसका आशय धोखा देने का नहीं था, परन्तु यदि कोई वयस्कता प्राप्त लड़की विवाह के वचन के आधार पर स्वयं को शारीरिक सम्भोग के लिए प्रस्तुत करने को तैयार हो तब यदि वह गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी।
यह उल्लेखनीय है कि अपने माल की अति प्रशंसा छल के अन्तर्गत नहीं आयेगी। परन्तु यदि विक्रय किया हुआ माल निरूपित माल से पूर्णतः भिन्न हो तथा विक्रेता के वर्णनानुसार मेल न खाता हो तो वह छल का अपराध माना जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि चेक अनादृत (Dishonoured) हो जायेगा। किसी अन्य व्यक्ति को वह चेक उस रकम की अदायगी के रूप में देता है तो वह छल के अपराध का दोषी होगा। यदि कोई व्यक्ति रेल के निचले दर्जे का टिकट लेकर ऊँचे दर्जे में यात्रा करता है या निर्धारित वजन से अधिक वजन के लिए लगेज किराया देने से बचने के लिए अपने सामान का कुछ भाग एक सहयात्री को अन्तरित करता है तो वह छल का अपराध नहीं होगा। यदि कोई एक कोरे कागज पर किसी व्यक्ति का अंगूठा निशानी लेता है तो वह छल का प्रयास हो सकता है तथा यदि उस कागज पर कुछ लिखा नहीं जाता तो वह न तो छल होगा न हो छल का प्रयास
छल तथा कूट-रचना में अन्तर
(Distinction between Cheating and Forgery)
छल तथा कूट- रचना (Forgery) दोनों में एक पक्षकार का आशय बेईमानीपूर्वक तथा कपटपूर्वक ढंग से अनुचित लाभ उठाना होता है। छल तथा कपट दोनों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कपटपूर्ण आचरण के कारण नुकसान या हानि उठाता है।
छल तथा कूटरचना में निम्न अन्तर है –
छल (Cheating)
(1) छल की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में दी गई है।
(2) छल के अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे ( व्यक्ति को असत्य कथन कर कोई कार्य या कार्यलोप करने को उत्प्रेरित करता है।
(3) छल के अन्तर्गत किसी को प्रवंचना, मिथ्या कथन के आधार पर सम्पत्ति परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है।
कूट रचना (Forgery)
(1) कूटरचना (Forgery) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
(2) कूट रचना के अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से मिथ्या दसतावेज या दस्तावेजों के भाग को रचता है।
(3) कूटरचना (Forgery) के अन्तर्गत मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज या दस्तावेजों के भाग के आधार पर किसी सम्पत्ति या हक पर दावा किया जाता है या दावे के समर्थन में उस कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न 22 (ii) आपराधिक अतिचार से आप क्या समझते हैं? आपराधिक अतिचार तथा गृहभेदन में अन्तर स्पष्ट कीजिए? What do you understand by Criminal Trespass? Explain the difference between Criminal Trespass and House Breaking.
उत्तर– किसी कब्जाधारी की भूमि, भवन या परिसर पर अनधिकार प्रवेश ही अतिचार है भले ही कम समय का क्यों न हो। चूँकि यह कब्जे के विरुद्ध अपराध है अतः यह स्वामी द्वारा किरायेदार के विरुद्ध भी सम्भव है। विधिपूर्ण कब्जे की समाप्ति के पश्चात् कब्जा अनधिकृत हो जाता है तथा कब्जाधारी अतिचारी माना जाता है। इसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 परिभाषित करती है। इस परिभाषा के अनुसार जो कोई किसी ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे अथवा ऐसी सम्पत्ति में या ऐसी सम्पत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधि विरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्द्द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, वह आपराधिक अतिचार कहलाता है।
इस प्रकार आपराधिक अतिचार के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी का आशय किसी दूसरे के कब्जे में की सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर प्रवेश करना है। ऐसा करने का उसका आशय या तो कोई अपराध कारित करना होता है या ऐसी सम्पत्ति में या सम्पत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ इस आशय से बना रहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या कोई अपराध कारित करे। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं
(1) अभियुक्त का अपेक्षित आशय होता है जब वह किसी की सम्पत्ति में प्रवेश करता है।
(2) अभियुक्त अन्य की सम्पत्ति में विधिपूर्वक तरीके से प्रवेश करता है परन्तु विधि विरुद्ध आशय से वहाँ बना रहता है।
इस प्रकार इस अपराध के लिए दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, चूँकि आपराधिक अतिचार अभियुक्त के आशय पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ जहाँ अभियुक्त ने अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए पड़ोसी की भूमि पर अतिचार कर एक किनारे को काट दिया, जो सामान्य रूप से वह नहीं करता, यह मात्र सिविल अतिचार का उदाहरण है। कृष्ण बल्लभ मिश्र बनाम राज्य, 1974 क्रि० लॉ ज० 434 इलाहाबाद के बाद में अभियुक्त जो एक स्कूल समिति का उपाध्यक्ष था, स्कूल परिसर में गया जो प्रधानाध्यापक के कब्जे और नियन्त्रण में था, और उसने दो विद्यार्थियों को पीटा और उसकी इच्छा प्रधानाध्यापक को भी पीटने की थी, वह आपराधिक अतिचार का दोषी होगा। अब्दुल नूर लस्कर बनाम राज्य, 1985 क्रि० लॉ ज० (1959) गौहाटी के बाद में अभियुक्त ने एक विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने कब्जे के अधिकार का प्राख्यान किया और उसने ऐसा दस्तावेज भी पेश किया जो यह दर्शाता था कि उसका उसमें कुछ अधिकार है, जब तक कि न्यायालय ही उसे बेदखल न कर दे, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह आपराधिक अतिचार का दोषी नहीं था क्योंकि वह सद्भावपूर्ण रूप से कार्य कर रहा था और इस प्रकार उसका अपेक्षित आशय नहीं था परन्तु जहाँ अभियुक्तों ने परिवादी के कब्जे की भूमि में प्रवेश किया और उसकी खेती को नुकसान पहुँचाया तब उनका कार्य सद्भावपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अतः वह आपराधिक अतिचार का दोषी माना जायेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 445 गृह-भेदन को परिभाषित करती है। गृह अतिचार का अपराध उस स्थिति में गृहभेदन का अपराध बन जाता है जब धारा 445 में उपबन्धित छ रीतियों में से किसी एक रीति से गृह में प्रवेश या बहिर्गमन किया गया हो।
आपराधिक अतिचार तथा गृह भेदन में अन्तर
आपराधिक अतिचार
(1) आपराधिक अतिचार की परिभाषा धारा 441 में दी गई है।
(2) किसी व्यक्ति की भूमि, भवन या परिसर पर बिना किसी विधिक औचित्य के अनधिकार प्रवेश करना आपराधिक अतिचार कहलाता है।
(3) गृह अतिचार किसी भूमि, भवन या परिसर पर प्रवेश मात्र है, चाहे कोई अन्य कार्य न भी किया गया हो।
गृह भेदन
(1) गृह भेदन की परिभाषा धारा 445 के अन्तर्गत दी गई है।
(2) जब कोई व्यक्ति किसी के घर में या उसके किसी भाग में इस धारा में वर्णित छः प्रकार से प्रवेश करता है तो वह गृह-भेदन करता है।
(3) गृह भेदन में गृह में प्रवेश करने के पश्चात् कोई सकारात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।
प्रश्न 23. (i) बल्वा करना क्या है? बल्वा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।
What is Rioting? Discuss the essential elements of Rioting.
उत्तर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 146 में बल्वा को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 146 के अनुसार, “जब विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के लिए दोषी होता है। बल्वा के आवश्यक तत्व-बल्वा के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है –
(1) पाँच या अधिक व्यक्तियों का विधि-विरुद्ध जमाव निर्मित होना चाहिए,
(2) वे किसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हों;
(3) उन्होंने आशयित सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दो हो
(4) उस अवैध जमाव ने या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो;
(5) ऐसे बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो।
परमेश्वर सिंह बनाम सम्राट (1899) 4 सी० डब्ल्यू० एन० 345 के बाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा केवल बल का प्रयोग किये जाने मात्र से जमाव के सदस्य बल्वे के अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि बल प्रयोग किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया था। यदि जमाव का सामान्य उद्देश्य विधि-विरुद्ध न हो, तो उसके किसी सदस्य द्वारा बल प्रयोग किया जाने पर भी उसे ‘बल्वा’ नहीं माना जाएगा।
शेरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1991 एस० सी० 2246 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बल्चे के मामले में केवल ऐसे अभियुक्तों की हो दोषसिद्धि की जानी चाहिए जिनको उपस्थिति प्रारम्भ से अन्त तक बनी रही है तथा उन्होंने हिंसा या बल प्रयोग में वास्तव में भाग लिया हो।
प्रश्न 23 (ii) दंगा क्या है? दंगा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।
What is Affray? Discuss the essential elements of Affray.
उत्तर- दंगा (Affray)- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 159 के अनुसार, “जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लड़कर लोक-शान्ति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वह ‘दंगा’ करते हैं।
दंगा (affray) शब्द फ्रेंच भाषा के (Affraier) शब्द से बना है जिसका अर्थ है, आतंकित करना यानि जनता को आतंकित करना।” दंगा के अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं –
(1) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई
(2) लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो;
(3) उनकी लड़ाई से लोकशान्ति को व्यवधान पहुँचे।
दो या दो से अधिक व्यक्ति- दंगा के अपराध के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उनकी संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।
सार्वजनिक स्थान पर लड़ना- दंगा निर्मित करने हेतु आवश्यक है कि लड़ाई किसी सार्वजनिक या लोक स्थान में हो। सार्वजनिक स्थान वह स्थान है जहाँ जनता बिना किसी आज्ञा या बाधा के आती-जाती है।
उदाहरण– रेलवे प्लेटफार्म, सिनेमा हाल, बाजार, सार्वजनिक मूत्रालय आदि।
जगन्नाथ साह (1937) ओ० डब्ल्यू० एन० 37 के बाद में दो भाई एक कस्बे की सड़क पर आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा एक दूसरे को गालियाँ तक दे थे। वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गयी थी तथा यातायात बिल्कुल बंद हो गया था किन्तु आघातों का आदान-प्रदान नहीं हुआ था। यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव में दंगा नहीं कारित हो सकता।
लोकशान्ति को भंग करे– दंगा के अपराध को गठित करने के लिए सार्वजनिक स्थान में केवल लड़ाई ही पर्याप्त नहीं है अपितु ऐसी लड़ाई लोक-शांति को व्यवधान पहुँचाए। पोदन (1962) 1 क्रि० एल० जे० 339 के बाद में कहा गया कि लड़ाई सामान्य उत्तेजना एवं व्यवधान उत्पन्न करे और मात्र लोक असुविधा कारित करना पर्याप्त नहीं है।
प्रश्न 24. पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना या द्विविवाह क्या है? द्विविवाह के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए।
What is marrying again during lifetime of husband or wife or Bigamy? Discuss the essential elements of Bigamy.
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 494 में द्विविवाह को परिभाषित किया गया है। धारा 494 के अनुसार-“जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा, जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगो, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।”
अर्थात् यह धारा द्विविवाह को प्रतिबन्धित करती है और उसे एक दण्डनीय अपराध मानती है। पति-पत्नी के बीच किसी वैध विवाह के अस्तित्व में होते हुए उनमें से कोई किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकेगा जब तक कि वह वैध विवाह किसी कारण से समाप्त नहीं हो गया हो या वैध नहीं रह गया हो। यह धारा प्रत्येक हिन्दू पारसी तथा ईसाई के प्रति लागू होती है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री परन्तु मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत इस धारा के उपबन्ध केवल मुस्लिम महिला के प्रति लागू होते हैं तथा मुस्लिम पुरुष एक समय चार पत्नियाँ तक रख सकता है।
आवश्यक तत्व – धारा 494 के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं
(1) जिस समय अभियुक्त ने दूसरा विवाह किया हो। उस समय उसका पति/पत्नी ने जीवित हो और उनके बीच वैध विवाह अस्तित्व में हो।
(2) अभियुक्त द्वारा किया गया दूसरा विवाह पहली पत्नी अथवा पति के जीवन काल में किये जाने के कारण उस विधि के अन्तर्गत शून्य हो जिसके द्वारा अभियुक्त प्रशासित है।
कंवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए० आई आर 1966 एस० सो० 614 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 494 के अन्तर्गत अपराध के लिए यह सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है कि पुनः विवाह को सभी आवश्यक रीतियों का पालन किया गया है। अभियुक्त द्वारा केवल पुनः विवाह के तथ्य को स्वीकार किया जाना मात्र जारकर्म या द्विविवाह के अपराध के लिए पर्याप्त साध्य नहीं माना जाएगा।
धारा 494 के अपवाद – धारा 494 में दो अपवाद हैं –
(1) यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी विवाद को शून्य घोषित कर दिया है तो पक्षकारों द्वारा द्विविवाह किया जा सकता है।
(2) यदि विवाह के किसी पक्षकार ने पति अथवा पत्नी के बारे में निरन्तर 7 वर्ष तक कुछ भी नहीं सुना हो तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पुनः विवाह किया जाना धारा 494 के अन्तर्गत अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा।
अर्थात् पति-पत्नी के बीच वैध तलाक हो जाने के पश्चात् पुनः विवाह कर सकते हैं।
प्रश्न 25. जारकर्म क्या है? जारकर्म के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं जारकर्म तथा द्विविवाह, जारकर्म तथा बलात्संग में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
What is Adultery? Discuss the essential elements of Adultery and explain the diffrence between Adultery and Bigamy, Adultery and Rape.
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497 में जारकर्म को परिभाषित किया गया है। धारा 497 के अनुसार-जारकर्म से तात्पर्य ऐसे संभोग से है जो किसी पुरुष द्वारा अन्य की पत्नी के साथ उस व्यक्ति को सम्मति के बिना अथवा उसकी मौन स्वीकृति के बिना किया जाता है। जिस महिला के साथ संभोग किया जाय वह किसी व्यक्ति की विधितः विवाहिता पत्नी हो
यदि कोई व्यक्ति (पुरुष) किसी अविवाहिता या विधवा या तलाकशुदा स्त्री के साथ संभोग करता है, या उस स्त्री के पति की सम्मति या मौन स्वीकृति से उस स्त्री से संभोग करता है तो उसे जारकर्म के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा।
धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म के अपराध का संज्ञान केवल विवाहिता महिला के पति की सम्मति या मौन स्वीकृति के बिना किसी पुरुष द्वारा उस महिला से संभोग किये जाने की दशा में ही लिया जा सकता है तथा इसके लिए केवल पुरुष को हो दण्डित किया जा सकता है। अतः इस धारा के अनुसार, जारकर्म एक ऐसा अपराध है जो कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी पति के विरुद्ध उसकी पत्नी के प्रति किया जाता है।
जारकर्म के आवश्यक तत्व – धारा 497 के अन्तर्गत जारकर्म के अपराध के मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध निम्नलिखित बातों का साबित किया जाना आवश्यक है
(1) किसी पुरुष द्वारा किसी ऐसी महिला के साथ संभोग किया गया हो, जो किसी अन्य की पत्नी हो या जिसके बारे में वह जानता हो या उसे विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वह स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है।
(2) अभियुक्त द्वारा ऐसा संभोग उस स्त्री के पति को सम्मति या मौन-सहमति के बिना किया गया हो।
(3) ऐसा संभोग-कृत्य बलात्संग की कोटि में आता हो।
सौमेत्री विष्णु बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1985 एस० सी०: 148 के बाद में भाग 497 को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अन्तर्गत समानता के अधिकार के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दो गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धारा 497 के अन्तर्गत व्यथित पति को जारकर्म करने वाले व्यक्ति को आरोपित करने का अधिकार है परन्तु जारकर्म करने वाले व्यक्ति की पत्नी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः यहाँ लिंग विभेद किया गया है, किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुरुष प्रधान भारतीय समाज में जो महिला जारकर्म का शिकार हुई हो वह वस्तुत: एक पीड़ित स्त्री होती है न कि अपराध की रचयिता इस पृष्ठभूमि में सम्भवतः अभी जारकर्म में सहभागी स्त्री को अपराधी के रूप में दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा अतः धारा 497 संवैधानिक है।
जारकर्म तथा द्विविवाह (Adultery and Bigamy) में अन्तर –
जारकर्म (Adultery)
(1) जारकर्म एक लैंगिक सम्भोग या ( मैथुन से सम्बन्धित अपराध है। इसमें किसी की विवाहिता स्त्री से मैथुन किया जाना आवश्यक है।
(ii) यह अपराध इस जानकारी के साथ किया जाता है कि, जिससे मैथुन किया जा रहा है, वह दूसरे की विवाहिता पत्नी है।
(iii) यदि पति की सहमति से उनकी पत्नी के साथ मैथुन किया जाता है तो जारकर्म का अपराध गठित नहीं होता।
(iv) जारकर्म के लिए पाँच वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
द्विविवाह (Bigamy)
(i) द्विविवाह एक वैवाहिक अपराध है। इसमें एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया जाना आवश्यक है।
(ii) इसमें पूर्व-पत्नी का जीवित होना आवश्यक है।
(iii) इसमें पति या पत्नी की सहमति का कोई महत्व नहीं होता।
(iv) द्विविवाह के लिए सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
जारकर्म तथा बलात्संग (Adultery and Rape) में अन्तर
जारकर्म (Adultery )
(i) जारकर्म विवाह के विरुद्ध अपराध है तथा यह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ किया जाता है।
(ii) जारकर्म अविवाहिता, तलाकशुदा या विधवा के साथ नहीं हो सकता।
(iii) जारकर्म का अपराध किसी भी स्थिति में एक पति अपनी ही पत्नी के साथ नहीं कर सकता।
(iv) जारकर्म का अपराध पत्नी की सहमति से भी सम्भव है।
(v) जारकर्म में पीड़ित पक्षकार पति होता है।
(vi) जारकर्म अपेक्षाकृत कम गम्भीर अपराध है तथा इसके लिए पाँच वर्ष के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
(vii) जारकर्म में हिंसा या जोर-जबरदस्ती आवश्यक नहीं है।
बलात्संग (Rape)
(i) बलात्संग शरीर के विरुद्ध अपराध है तथा यह किसी भी स्त्री के साथ बल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है।
(ii) बलात्संग किसी भी स्त्री के साथ हो सकता है, चाहे वह अविवाहिता, तलाकशुदा, विधवा या विवाहिता कोई भी हो।
(iii) बलात्संग अपनी ही पत्नी के साथ सम्भव है यदि पत्नी की वर्ष से कम हो । आयु पन्द्रह
(iv) बलात्संग का अपराध सदैव किसी भी स्त्री की सहमति के बिना होता है।
(v) बलात्संग में पीड़ित पक्षकार एक स्त्री होती है।
(vi) बलात्संग एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है जिसे आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास या आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
(vii) बलात्संग में जोर-जबरदस्ती या बल प्रयोग की महत्व दिया जाता है।
प्रश्न 26. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित विधियों की चर्चा करें।
Discuss the law relating to offences against women?
उत्तर – भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में कई धाराओं में उपबन्ध किया गया है। जैसे –
धारा 312 से 314 तक महिलाओं की सहमति के विरुद्ध गर्भपात करने को अपराध घोषित करती हैं। धारा 354 स्त्री की लचा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग को निषिद्ध करता है। धारा 366 विवाह करने के लिए स्त्री को व्यपहृत करना तथा धारा 366 क, ख किसी अप्राप्तवय लड़की तथा विदेशों से लड़की के उपापन तथा आयात को अपराध घोषित करती है, धारा 372, 373 वेश्यावृत्ति को रोकती है।
महिलाओं की सहमति के विरुद्ध गर्भपात कारित करना– जो कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक न किया जाये तो वह इसके अधीन दण्डनीय है और यदि स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करता है तो धारा 313 के अधीन कठोर कारावास से दण्डित होगा। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाय और यदि गर्भवती स्त्री की सहमति न ली गयी हो तो आजीवन कारावास से दण्डित हो सकता है।
स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – इस धारा 354 के अधीन किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अपराधी का आशय स्त्री की लज्जा भंग करना होना चाहिए। किसी स्त्री या उसकी उपस्थिति में कोई ऐसा कार्य जो मानव जाति की सामान्य धारणा के अनुसार काम भावना का संकेत दे तो वह कार्य इस धारा के अधीन दण्डनीय माना जायेगा। स्त्री को लब्बा का सार उसका लिंग होता है और अभियुक्त का आपराधिक आशय या ज्ञान इस विषय का मर्म है।
स्त्री को अपहृत करना- विवाह आदि करने के लिए किसी भी स्त्री का अपहरण किया जाये करना एक अपराध है। अपराधी का आशय उसको इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह कियो व्यक्ति से करना, या अयुक्त सम्भोग करने के लिए उसको विवश करना होना चाहिए। यदि अपराधी का आशय ऐसा न हो तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी सम्भावना हो सकती है।
अप्राप्तवय लड़की तथा विदेश से लड़की का आयात करना- जब 18 वर्ष मे कम आयु को अप्राप्तवय लड़कों को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी मादक पदार्थ द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है तो यहाँ अभियुक्त का आशय उस लड़की को अन्य व्यक्ति से सम्भोग करने के लिए विवश या विलुप्त करना होना चाहिए या इसकी सम्भावना का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार विदेश आदि से 21 वर्ष से कम की लड़की का आयात करना अपराध है। सैय्यद अहमद बनाम राज्य, 1993 क्रि० लॉ ज० 1920 आन्ध्र प्रदेश के बाद में अभियुक्त एक अप्राप्तवय लड़की को उसकी माँ की अभिरक्षा से ले गया और उसके साथ बलात्संग किया और यह साबित हो गया कि उसकी आयु घटना के समय पन्द्रह वर्ष थी तथा अभियुक्त ने उस लड़को से उसकी आयु के बारे में एक मिथ्या शपथ-पत्र प्राप्त किया और धमकी के अन्तर्गत उससे विवाह किया तथा उसके साथ बलात्संग किया। न्यायालय ने यह धारित किया कि अभियुक्त धारा 366 क के अधीन दोषी थे। इस प्रकार किसी अभियुक्त को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके विरुद्ध अपेक्षित आशय या ज्ञान सावित न हो जाय।।
वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना– वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना, भाड़े पर देना आदि इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है। इसके अनुसार जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से बेचेगा, भाड़े पर देगा या उसे वेश्यावृत्ति करने या किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश करेगा या किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लायेगा दण्डनीय होगा। अयुक्त सम्भोग से तात्पर्य है ऐसे व्यक्तियों से मैथुन करना जो विवाह से संयुक्त नहीं हैं। अपेक्षित आशय या ज्ञान के साथ 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को देवदासी के रूप में अर्पित करना इस भाग के अधीन अपराध होगा।
प्रश्न 27. कूटरचना एवं मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचना को परिभाषित एवं स्पष्ट कीजिए।
Define and explain forgery and making false electronic record.
उत्तर- कूटरचना (Forgery)- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 463 में कूट रचना’ को परिभाषित किया गया है। धारा 463 के अनुसार, “जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति, सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है।”
सुशील सूरी बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, ए० आई० आर० (2011) सु० को० 1713 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथन किया कि धारा 463 में दी गयी कूटरचना को परिभाषा के अनुसार इस अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं –
(1) मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना करना (2) इस प्रकार के दस्तावेज की रचना इस आशय से की जाए कि
(i) किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति कारित करने हेतु, या
(ii) किसी हक या दावे के समर्थन हेतु या
(iii) किसी व्यक्ति से सम्पत्ति छुड़ाने हेतु या
(iv) किसी व्यक्त या विवक्षित संविदा करने हेतु या
(v) कपट करने के लिए या कपट की सम्भावना उत्पन्न करने हेतु।
मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना (धारा 464) – मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना से तात्पर्य प्रथमतः जो बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से –
(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है,
(ख) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है,
(ग) किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है।
(घ) दस्तावेज का निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का अधिप्रमाणन द्योतन करने बाल कोई चिन्ह लगाता है।
कि यह विश्वास किया जाये कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाया जाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता है या,
द्वितीय:- अभियुक्त किसी दस्तावेज के या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तित उसके द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हों या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, अथवा,
तृतीयः – जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को या परिवर्तन के रूप को चित्तविकृत या मत्तता की हालत में होने के कारण जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक • अभिलेख का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्तान्तरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना कारित करता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किया जाना कारित करता है।
जैसे-‘क’ के पास ‘ख’ द्वारा ‘ग’ पर लिखा हुआ 50,000 रुपये का एक प्रत्ययपत्र है। ‘ग’ से कपट करने के लिए ‘क’ 50,000 रुपये में एक शून्य चढ़ा देता है और उस राशि को 5,00,000 इस आशय से बना देता है कि ‘ग’ यह विश्वास कर ले कि ‘ख’ ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था। ‘क’ ने कूटरचना की है।
कूटरचना एक ऐसा साधन है जिसका लक्ष्य किसी व्यक्ति को धोखा देना होता है। छल के अपराध की भांति कूटरचना में भी मिथ्या व्यपदेशन का तत्व विद्यमान रहता है लेकिन छल मुख्यतः मौखिक होता है जबकि कूटरचना अनन्यतः लिखित होता है।
आर० बनाम काली प्रसाद बनर्जी, ए० आई० आर० 1915 कल० 786 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम उसके द्वारा अधिकृत किये गये बिना तार पर उसके हस्ताक्षर करना कूटरचना की कोटि में नहीं आता, यदि उसमें उसे कोई क्षति पहुँचाने का आशय न हो और वास्तविक रूप से कोई क्षति न पहुँची हो।