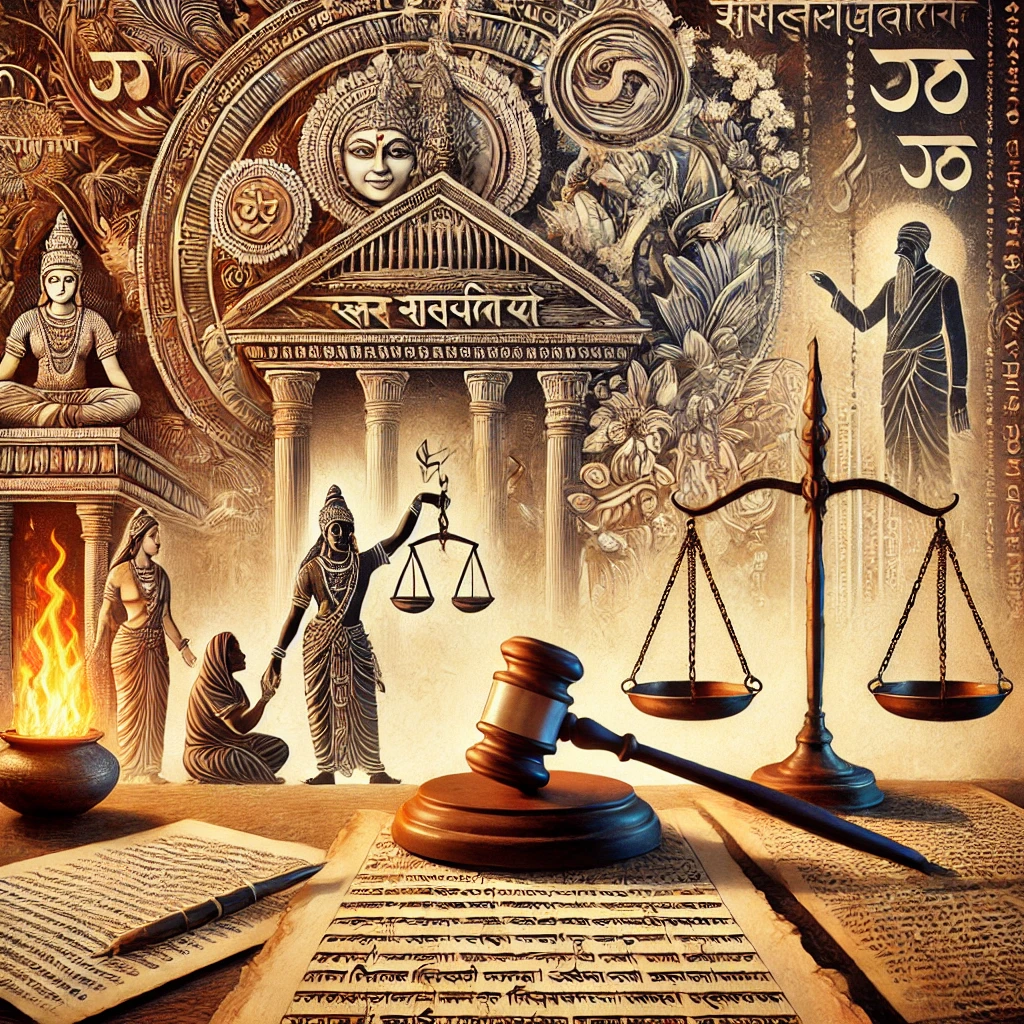– प्रथम सेमेस्टर-
HINDU LAW Long Answer
प्रश्न 1. हिन्दू विधि के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। इन स्त्रोतों में प्रधा (रूढ़ि) के महत्व की व्याख्या करें। हिन्दू विधि में वैध प्रथा की आवश्यकता क्या है?
Discuss the main sources of Hindu Law. Discuss the importance of custom in this sources. What are the essential conditions of valid custom in Hindu Law?
उत्तर- हिन्दू विधि के मुख्य स्रोत हिन्दू विधि के स्रोतों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-
(1) प्राचीन स्रोत, (2) आधुनिक स्रोत
प्राचीन स्रोतों में मुख्यत: पाँच स्रोत आते हैं- 1. श्रुति, 2. स्मृति, 3. निबन्ध, 4. भाष्य, में 5. प्रथा।
आधुनिक स्रोतों के अन्तर्गत निम्न तीन स्रोत सम्मिलित किये गये हैं- 1. साम्या, न्याय तथा सद्विवेक, 2. न्यायिक निर्णय, 3. विधायन (Legislation)
स्रोत का अर्थ है हिन्दू विधि का उद्गम इस प्रकार यहाँ हमें यह विचार करना है कि है हिन्दू विधि किस प्रकार अस्तित्व में आयी अर्थात् वर्तमान हिन्दू विधि को अस्तित्व में आने से पूर्व किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। हिन्दू विधि अपने वर्तमान रूप में आने से पूर्व जिस-जिस अवस्था में थी, उन्हें हिन्दू विधि का उद्गम या स्रोत माना जा सकता है।
हिन्दू विधि के प्राचीन स्त्रोत– 1. श्रुति, 2. स्मृति, 3. पुराण, 4 निबन्ध तथा भाष्य, 5. प्रथाय
(1) श्रुति (Srutis) – मनु के अनुसार श्रुति अर्थात् जो सुना गया है सिद्धान्ततः हिन्दू विधि के सर्वोच्च तथा प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। श्रुति को दैववाणी या आकाशवाणी माना। जाता है। श्रुति का अर्थ है जो सन्तों द्वारा सुना गया। श्रुतियों को चार वेदों, छः वेदांगों तथा अठारह उपनिषदों में संग्रहित किया गया है। इसमें मुख्यतः धार्मिक रीतियों के अनुष्ठानों तथा सत्य ज्ञान प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने के साधनों के बारे में वर्णन मिलता है। वेद मुख्यत: हिन्दू विधि के प्रधागत स्रोत माने जाते हैं। ये सबसे अधिक प्राचीन हैं तथा इन्हें आकाशवाणी या दैववाणी की प्रत्यक्ष घोषणाओं के रूप में मान्यता मिली है। यद्यपि वेदों को त्रुटिहीन माना जाता है तथा वेद चार हैं- 1. ऋगवेद, 2. यजुर्वेद, 3. सामवेद, 4. अथर्ववेद परन्तु आधुनिक समय में इनका व्यावहारिक मूल्य बहुत कम है।
(2) स्मृतियाँ (Smiritis)— स्मृति का अर्थ है जो कुछ स्मृत या याद है। स्मृतियों का आधार मुख्यतया वेद हैं। स्मृतियों के लेखक यह दावा नहीं करते कि स्मृतियाँ शब्दश: दैव वाणी ही हैं परन्तु उनका कहना है कि प्रथागत रूप से सुने गये दैवी नियम को उन्होंने संग्रहित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मृतियों का उद्गम दैवीय न होकर मानवीय है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अग्रणी है। मनुस्मृति के पश्चात् याज्ञवल्क्य नारद, परासर तथा बृहस्पति की स्मृतियों का स्थान विधि को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्रमुख है।
स्मृतियाँ दो प्रकार की हैं- (1) भाष्य रूप में जिसके लेखक गौतम बौधायन, वशिष्ट तथा परासर हैं। इन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है। (गद्य रूप में) (2) जो स्मृतियाँ श्लोकों में हैं, उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनु, क्य, नारद,
विष्णु इसके लेखक हैं। (श्लोकों में)
(3) पुराण (Purana)– मिश्र ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपने भाष्य में यह लिखा है कि विधि के विषय में पुराण अधिकारिक नहीं है। गंगा सहाय बनाम लेखराज में यह निर्णय दिया गया है कि पुराण का स्थान विधि के स्रोत के रूप में श्रुति तथा स्मृति के पश्चात् आता है। पुराण को किन्हीं विधिवेत्ताओं ने पाँचवां वेद माना है।
(4) भाष्य तथा निबन्ध-भाष्य वे हैं जिनमें स्मृतियों की टीका की गई है। भाष्यकारों ने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने नये कानून बनाये, उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधियों का संकलन एवं उनकी व्याख्या की और उस विधि को स्थापित किया। कुछ भाष्य राजा के कहने पर या उनको संरक्षकता में लिखे गये। प्रिवी कौंसिल का यह कथन उपयुक्त माना जाता है कि ये भाष्य विधि का निर्वचन, जैसा कि स्मृतियों में उल्लिखित था, करते हुए उसमें इस प्रकार के परिवर्तन लाये जो कि प्रचलित प्रथाओं के सम्बन्ध में उस विशेष क्षेत्र में आवश्यक हो गया था जहाँ उनकी रचना की गई। आत्माराम बनाम बाजीराव, (1935) 62 1.A. 139 के बाद में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि जहाँ स्मृति को विधि तथा भाष्य की विधि में विरोध हो, वहाँ भाष्य की विधि मान्य होगी। प्रमुख भाष्य इस प्रकार हैं-
(1) दाय भाग जीमूतवाहन द्वारा
(2) विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा
(3) मित्रमिश्र द्वारा वीर मित्रोदय
(4) वाचस्पति द्वारा विवाद-चिन्तामणि
(5) चन्द्रशेखर द्वारा विवाद- रत्नाकर इत्यादि।
(5) प्रथा (Custom)-प्रथाएँ ऐसे नियमों को कहते हैं जिन्हें किसी विशिष्ट स्थान विशिष्ट परिवार या विशिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में लम्बी अवधि के प्रयोग से विधि से बल प्राप्त हो गया हो। प्रिवी कौंसिल के अनुसार प्रथा किसी विशिष्ट परिवार या जिले में प्रचलित नियम हैं लम्ब विधि के प्रयोग के कारण कानून से बल प्राप्त हो गया है। प्रथा को वैध होने के लिए प्रथाएँ प्राचीन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, युक्तियुक्त (उचिव) होतो चाहिए तथा विधि के सामान्य नियमों के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। प्राचीन लेखकों ने प्रमा के बाध्यकारी लक्षण को स्वीकार किया है तथा यह माना है कि प्रत्येक प्रयाएँ खोई हुई देव वाणियाँ ही हैं। आधुनिक युग में भी प्रथाओं को उतने ही प्रभावशाली ढंग से स्वीकार किया गया है। रामानन्द के बाद में प्रिवी कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि प्रथा का सबूत लिखित विधि के लेख से भी ऊपर माना जाता है। यह कहा जाता है कि स्मृतियों तथा भाष्य का आधार प्राचीन प्रथाएँ ही रही हैं। जिन मामलों में न ही स्मृतियाँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं एवं न ही प्रथाएँ उनमें निर्धारित नियम के सम्बन्ध में विधि ही सहायता करती है।
अन्य स्रोत (Other sources) आधुनिक स्रोत- (1) विधायन (Legislation) (2) न्यायिक निर्णय (Precedents). (3) न्याय, साम्या तथा सद्विवेक (Justice, Equity and Good conscience) सम्मिलित हैं।
(1) विधायन (Legislation)- ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुछ ऐसे अधिनियम पारित किये गये जिन्होंने मूल हिन्दू विधि को समय-समय पर संशोधित तथा अनुपूरित किया है जैसे बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम, 9129, हिन्दू गेम्स ऑफ लर्निंग अधिनियम, 1930, हिन्दू स्त्री सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 आदि। स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दू विधि के सम्बन्ध में चार प्रमुख अधिनियम पारित किये गये जिनके अन्तर्गत भारतीय संसद ने विवाह, दत्तक, संरक्षकता तथा उत्तराधिकार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर हिन्दू विधि के इस क्षेत्र को सुनिश्चितता तथा बोधगम्यता प्रदान की। जैसे-(1) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (2) हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 आदि।
(2) न्यायिक निर्णय (Judicial Decision)-ऐसे निर्णय जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये जाते हैं वे उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लम्बित वादों में नजीर का कार्य करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। वास्तव में विधायन तथा न्यायिक निर्णय हिन्दू विधि के स्रोत नहीं हैं। इन्होंने हिन्दू विधि को संशोधित करने तथा उसमें निहित खामियों को दूर करने का कार्य किया है। न्यायालय का कार्य विधि का निर्माण करना नहीं बल्कि न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करके विधि को सुनिश्चित करना है। न्यायिक निर्णयों ने मूल हिन्दू विधि को संशोधित किया है तथा उसकी खामियों को दूर किया है। अतः हिन्दू विधि के वर्तमान स्वरूप के लिए न्यायिक निर्णयों ने कुछ सीमा तक स्रोत का कार्य किया है।
उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान काल में विवाह, दत्तक ग्रहण, स्त्री-धन आदि के सम्बन्ध में ऐसे अनेक निर्णय दिये हैं जिनसे न केवल विधि के निर्वचन का प्रश्न हल हुआ वरन् नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ। उदाहरण के लिए प्रतिभारानी बनाम सूरज कुमार, ए० आई० आर० 1985 एस० सी० 628 का निर्णय स्त्रीधन के सम्बन्ध में पूर्णतया नया सिद्धान्त प्रस्तुत में करता है।
(3) न्याय, साम्या तथा सद्विवेक (Equity, Justice and Good Conscience) – भारत में साम्या का उद्गम हिन्दू काल में भी मिलता है। इस समय के विधिज्ञ पुराने नियमों एवं विधियों की व्याख्या करने में तथा नवीन नियमों को प्रतिपादित करने में साम्या का सहारा लेते हैं। विभिन्न नियमों में एक बिन्दु पर मतभेद के समय उसका समाधान करने हेतु साम्या का सहारा लिया जाता था तथा यह विचार किया जाता था कि परिस्थितियों में क्या उचित होगा जैसे स्मृतियों के मध्य मतभेद होने पर उसका समाधान तर्क, न्याय तथा साम्या के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता था।
इस प्रकार हम हिन्दू विधि के स्रोतों को दो भागों में बाँट सकते हैं। प्रथम, वे जो प्राचीन स्रोत हैं जैसे- श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्य, प्रथा आदि। यही प्राचीन हिन्दू विधि के वास्तविक तथा मूल स्रोत हैं। इनसे ही प्राचीन हिन्दू विधि का उद्गम हुआ। इन्हीं में हिन्दू वर्ग के आचरण तथा व्यवहार के नियमों का उल्लेख था, परन्तु दूसरा स्रोत, जिन्हें आधुनिक स्रोत कहते हैं, इन्हें वास्तविक स्रोत नहीं माना जाता परन्तु प्राचीन या मूल हिन्दू विधि में व्याप्त मतभेद, खामियाँ तथा गलतियों को दूर करने में इनका महत्व कम नहीं है। सोनों में हिन्दू विधि की प्रान्तियों तथा परस्पर विरोधों को दूर करके उसे निश्चितता तथा व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया।
प्रथा (रूड़) -को किसी विशिष्ट परिवार या जनपद के उन नियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे लम्बे समय तक प्रयोग में प्रचलित रहने के विधि का बल प्राप्त हो गया है। मानव के प्रारम्भिक इतिहास में विधि का मुख्य स्रोत हो रही है। भारतीय विधि में विधि के विकास में रूढि भूमिका को सदैव स्वीकार किया गया। स्मृतिकारों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि विवादों पर निर्णय लेते समय राजा को रूढ़िगत नियम लागू करने चाहिए।
मानव जीवन के विकास में पारस्परिक संघर्ष से बचने तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक समझा गया कि समाज के सभी लोग मानव आवरण के प्राथमिक नियमों के अनु आचरण करें। इसी आवश्यकता से कुछ मूलभूत नियमों का विकास हुआ जिसे मानव समाज के कोपभाजन के भय से अपने आचरण में स्थान देने लगा। यही मानव आवरण लगातार पालन के आधार पर सुस्थापित नियम बन गये जिन्हें दिया प्रथा का नाम दिया गया। मनु ने भी रूड़ियों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि किसी विवाद पर सदिगत, नियमों के अनुसार निर्णय देना राजा का कर्तव्य है। स्मृतिकारों में नारद का मत सर्वोपरि है। नारद के अनुसार रूढ़ि ही सब विवादों का निर्णय करती है। कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मुक्तराम लिंगम्, (1868) में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि हिन्दू विधि व्यवस्था में प्रभावित रूदि शास्त्रों में निर्धारित विधान एवं नियमों के प्रतिकूल होने पर भी मान्य हैं और प्रतिपादित की जा सकती हैं।
उदाहरण के रूप में एक ऐसी रूदि जिसके अन्तर्गत महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त है। तथा दक्षिण भारत में ब्राह्मण के कुछ वर्ग में अन्य की लड़की से विवाह करने प्रथा है। इन प्रथाओं को विधि द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। रूढ़ियाँ मुख्यत: तीन प्रकार की होती हैं
(1) स्थानीय रूढ़ि (देशाचार) (2) वर्ग रूद या सामाजिक (लोकाचार), (3) पारिवारिक रूढ़ियाँ (कुलाचार)
स्थानीय दि किसी विशेष देश, राज्य या जनपद तक सीमित होती है तथा उसके सभी निवासियों पर बाध्यकारी होती है। यहाँ तक कि किसी विशिष्ट शहर को भी पृथक् प्रथा हो सकती है।
सामाजिक रूढि किसी विशेष वर्ग रूढ़ि किसी विशिष्ट जाति, समुदाय या कष्ट वृद्धि का में प्रचलित होती है जैसे कृषि, व्यापार आदि क्षेत्रों में प्रचलित रूढ़ियाहैं
पारिवारिक रूड़ियाँ किसी विशिष्ट परिवार तक सीमित रहती हैं जैसे उत्तराधिकार तथा धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रचलित विधियाँ
रूड़ि की आवश्यक शर्ते– रूढ़ि को वैध होने के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं- (1) प्राचीनता (2) समरूपता तथा निरन्तरता (3) स्पष्टता तथा निश्चितता (4) युक्तियुक्तता (5) नैतिकता या लोकनीति के अनुकूल (6) रूड़ि विधि-विरुद्ध न हो (7) बाध्यता ।
(1) प्राचीनता (Ancient)- रूढ़ि को वैध होने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ि प्रचलन प्राचीन काल से या पुरातन समय से हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि स्मरणातीत समय से प्रचलन में हो। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3 (33) अनुसार रूढ़ि तभी मान्य होगी जब वह दीर्घकाल से चली आ रही हो। दीर्घकाल परिभाषा समयावधि के आधार पर देना कठिन है। न्यायालयों का मत है कि 100 वर्ष उससे अधिक की अवधि से चली आ रही रूढ़ि प्राचीन कहलायेगी। प्रिवी कौंसिल ने व्यक्त किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक रूढ़ि स्मरणातीत हो। कितनी प्रा रूढ़ि को मान्यता दी जानी चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित कि जाना चाहिए।
देवयात्री याची बनाम चिदाम्बरा (1954) के वाद में मद्रास उच्च न्यायालय के स प्रश्न उठा कि पच्चीस वर्ष पूर्व 1925 में एक पुरोहित विरोधी संस्था ने यह प्रचलन चल कि हिन्दू विवाह सभी प्रचलित अनुष्ठानों का त्याग कर सरल विधि से सम्पन्न होना चाहि इस आन्दोलन के अन्तर्गत प्रथम विवाह 1925 में हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय ने नि दिया कि सिर्फ पच्चीस वर्ष की अवधि रूढ़ि की स्थापना के लिए अपर्याप्त है।
(2) निरन्तरता (Continuity)- एक रूढ़ि के लिए वैधता प्रदान करने वा अनिवार्य शर्त निरन्तरता है। यदि यह साबित हो जाय कि एक रूढ़ि 200 वर्ष प्राचीन है। इस रूढ़ि को वैधता प्रदान करने हेतु यह भी साबित करना आवश्यक है कि जब से रूढ़ि प्रचलन प्रारम्भ हुआ तब से वह रूढ़ि निरन्तर प्रचलन में है। निरन्तरता का अभाव इस बात प्रमाण है कि रूढ़ि को परित्यक्त कर दिया गया है। यह परित्यजन जान-बूझकर भी हो सक है या आकस्मिक भी हो सकता है। किसी रूढ़ि का निरन्तर पालन न होना इस बात का साबित करता है कि वह रूढ़ि लुप्त हो गयी है। एक पारिवारिक रूढ़ि के सम्बन्ध में प्रि कौंसिल ने कहा कि यह हो सकता है कि जब रूढ़ि का निरन्तर पालन नहीं हो रहा है उत्तराधिकार में भी पारिवारिक रूढ़ि को परित्यक्त कर दिया गया है तथा उसका स्था सार्वजनिक उत्तराधिकार विधि ने ले लिया है। इस प्रकार निरन्तरता रूढ़ि की वैधता के लि उतना ही आवश्यक तत्व है जितना उसकी प्राचीनता।
(3) निश्चितता -निश्चितता रूढ़ि का तीसरा आवश्यक तत्व है। रूढ़ि तभी मान्य होगी जब यह सिद्ध हो जाय कि निश्चित रूप से रूढ़िगत नियम क्या है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि किसी विषय पर रूढ़िगत नियम लागू होता है। इसे रूढ़ि की रूपरेखा तथ उसके लागू होने के ढंग को निश्चितता के साथ प्रमाणित करना होगा। यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभित्यजन रूढ़ि यथार्थ में क्या है? इसका निश्चित रूप क्या है?
(4) युक्तियुक्तता (Reasonableness)- रूढ़ि को वैध होने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ि युक्तियुक्त हो। अयुक्तियुक्त (Unreasonable) रूढ़ि अमान्य तथा शून्य होती है। क्या युक्तिसंगत है क्या युक्तिसंगत नहीं है यह समाज की धारणाओं पर आधारित होता है। ये धारणाएँ या मान्यताएँ समाज तथा काल के साथ परिवर्तित होती हैं तथा एक रूढ़ि युक्तियुक है अथवा नहीं इसका निश्चय उस समाज की मान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है. जहाँ उस मान्यता पर प्रश्न उठे।
(5) रूढ़ि अनैतिक या लोकनीति के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए– अनैतिक रूढ़ियाँ अमान्य एवं शून्य होती हैं। नैतिक क्या है तथा अनैतिक क्या है इसका स्वरूप समाज में समय तथा काल के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक समाज की नैतिक मान्यताएँ भिन्न होती हैं। यदि रूढ़ि समयकालीन समाज की धारणाओं के अनुरूप नहीं है तो वह रूढ़ि अमान्य होगी। उदाहरण के रूप में यदि एक रूदि ऐसी है जिसके अनुसार पत्नी, पति की अनुमति के बिना उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर ले या पति, पत्नी को कुछ धन देकर विवाह-विच्छेद कर ले या अपने पुत्र को दूसरे परिवार में दत्तक देने वाला पिता धन की माँग करे यह सभी रूढ़ियाँ अनैतिक होने के कारण अमान्य तथा शून्य हैं। देव नारी की रूढ़ि जो दक्षिण भारत में प्रचलित है लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। इसी प्रकार पूजा स्थानों पर सार्वजनिक रूप से बलि देने वाली रूढ़ि भी लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। नर्तकियों में एक या अधिक पुत्री गोद लेने की रूढ़ि लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है। इसी प्रकार न्यासी द्वारा न्यास की सम्पत्ति को बेचने का अधिकार प्रदान करने वाली रूढ़ि लोकनीति के प्रतिकूल होने के कारण अमान्य है।
(6) रूढ़ि (विधान) विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए-व्यक्तिगत विधि चाहे मुस्लिम हो या हिन्दू विधि के अधीनस्थ रूढ़ियों को उन सम्बन्धित विधियों के अन्तर्गत (संहिताबद्ध करते समय) समाविष्ट कर लिया गया है। इसी प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में हिन्दू विवाह से सम्बन्धित रूढ़िगत अनुष्ठानों को विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है अतः अब यदि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी रूढ़ि है जो विवाह से सम्बन्धित है तथा हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रतिकूल है तो वह रूढ़ि विधि-विरुद्ध होने के कारण अमान्य होगी। इस प्रकार संहिताबद्ध हिन्दू विधि में रूढ़ि वहीं तक मान्य है जहाँ तक उसे अधिकृत रूप से मान्यता दी गई है।
(7) बाध्यता – रूढ़ि ऐसी होनी चाहिए जो कि इससे शासित हो रहे लोगों पर समान रूप से बाध्यकारी हो।
इस प्रकार रूढ़ि वे नियम हैं जो किसी विशिष्ट जनपद या परिवार में लम्बे समय तक प्रयोग में प्रचलित होने के कारण विधि का बल प्राप्त कर लिया है। रूढ़ि प्राचीन, निरंन्तर, स्पष्ट, निश्चित, युक्तियुक्त, नैतिक तथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। अब यह निर्विवाद रूप से सिद्धान्त बन चुका है कि एक स्पष्ट एवं निश्चित रूढ़ि को लिखित विधि पर भी वरीयता प्राप्त होगी।
प्रश्न 2. हिन्दू विधि की कौन-कौन सी शाखाएं हैं? स्पष्ट करें। मिताक्षरा तथा दायभाग में क्या अन्तर है?
How many branches of Hindu Law? Explain. What is the difference between Mitakshra and Daybhag?
उत्तर- हिन्दू विधि की शाखाएँ- रुचे पुत्री बनाम राजेन्द्र (1839) 2 एम० आई० ए० 132 के बाद में प्रिवी कौंसिल ने यह कहा था कि हिन्दू विधि में भिन्न-भिन्न शाखाओं का उदय भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित प्रथाओं के कारण हुआ। स्मृतियों के भाष्यकार मूल कृतियों की व्याख्या करते समय स्थानीय प्रथाओं एवं रूढ़ियों का तिरस्कार नहीं कर सकते थे और उन्होंने इसलिए स्थानीय प्रथाओं का अपने भाष्यों में अधिग्रहण कर लिया है। इस प्रकार स्मृतिकारों ने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित प्रथाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों में विधि के सिद्धान्तों को अपनी तरह से मोड़ने का सफल प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप अनेक शाखाओं का जन्म हुआ।
रामानन्द के बाद में पिवी कॉमिल ने ठीक ही कहा था कि हिन्दू विधि को विभिन शाखाओं में विधि के दूरस्थत एक हो है। जिस प्रणाली से इन शाखाओं का विकास हुआ इस प्रकार होती हैं जो कतियाँ सार्वजनिक अथवा अति सामान्य रूप से मान्य हुई। बाद में उन पर भाष्य के एक क्षेत्र में स्वीकार किये जाने और दूसरे क्षेत्र में अस्वीकार किये जाने के कारण परस्पर विरोधी सिद्धांतों वाली शाखाएँ उत्पन्न हुई।
हिन्दू विधि की मुख्यतया दो शाखाएँ हैं- प्रथम मिताक्षरा तथा दूसरा दायभाग दायभाग के सिद्धांत बंगाल में प्रचलित हैं तथा मिताक्षरा के सिद्धान्त भारत के अन्य भागों में इन दोन शाखाओं में मुख्य अन्तर यह है कि मिताक्षरा विधि शाखा बंगाल के अतिरिक्त समस्त देश में व्याप्त है। मिताक्षरा विधि के समर्थकों में भी अनेक उपशाखाएँ उत्पन्न हो गई। इन उपशाखा का जन्म छोटी-छोटी बातों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण हुआ, यद्यपि सिद्धांत रूप में ये सब एक ही हैं।
मिताक्षरा- मिताक्षरा के परिप्रेक्ष्य में डॉ० यू० सी० सरकार ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दू में यह लिखा है कि मिताक्षरा न केवल एक भाष्य है वरन् स्मृतियों पर एक प्रकार का निबन्ध है जो 11वीं शताब्दी के अन्त में अथवा 12वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखा गया था।
मिताक्षरा विधि की शाखा पाँच उपशाखाओं में विभाजित हुई है। ये उपशाखाएँ मिताक्षरा को सर्वोपरि प्रमाण मानती हैं, किन्तु वे कभी-कभी किसी मूल ग्रन्थ अथवा भाष्य विशेष को भी अधिमान्यता प्रदान करती हैं।
ये उपशाखाएँ इस प्रकार हैं –
बनारस शाखा- इस शाखा में उड़ीसा भी सम्मिलित है। पंजाब तथा मिथिला को छोड़कर यह शाखा समस्त उत्तरी भारत में व्याप्त है। इस शाखा के अन्तर्गत निम्न भाष्यों को मान्यता प्रदान की गयी है : 1. मिताक्षरा, 2. मित्रमिश्र द्वारा लिखित वीरमित्रोदय, 3. दत्तक मीमांसा, 4. निर्णय सिन्धु, 5. विवादताण्डव, 6. सुबोधिनी, 7. बालभट्टि।
मिथिला शाखा- सुरेन्द्र बनाम हरीप्रसाद 221 आई० ए० 418 के बाद में प्रिवी कौंसिल ने इस बात का समर्थन किया था कि-‘यह शाखा तिरहुत तथा उत्तरी बिहार में प्रचलित है। कुछ विषयों को छोड़कर इस शाखा की विधि मिताक्षरा की विधि है।’ इस शाखा में निम्नलिखित भाष्य मान्य हैं –
1. मिताक्षरा, 2. चन्द्रेश्वर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर, 3. वाचस्पति द्वारा लिखित विवाद चिन्तामणि, 4 स्मृतिसार, 6. मदन परिजात।
द्रविड़ अथवा मद्रास शाखा – हिन्दू विधि को मद्रास शाखा समस्त मद्रास में प्रचलित है। पहले यह शाखा तमिल, कर्नाटक तथा आन्ध्र उपशाखाओं में विभाजित थी। इस शाखा में निम्नलिखित कृतियों को मान्यता दी गई है –
1. मिताक्षरा, 2. देवनभट द्वारा लिखित स्मृति चन्द्रिका, 3. माधवाचार्य द्वारा लिखित पराशर माधवीय, 4. प्रतापरुद्रदेव द्वारा लिखित सरस्वती विलास 5. वीरमित्रोदय, 6. व्यवहार निर्णय, 7. दत्तक चन्द्रिका, 8. दाय विभाग, 9. केवलवयन्ती, 10. माधवी, 11. निर्णय सिन्धु, 12. नारद राज्य, 13. विवाद ताण्डव।
महाराष्ट्र अथवा बम्बई शाखा- यह शाखा पूरे बम्बई प्रदेश में प्रसिद्ध है जिसमें गुजरात, कनारा तथा वे प्रदेश प्रचलित हैं जहाँ मराठी बोली जाती है।
इस शाखा में निम्नलिखित ग्रन्थ है-1. मिताक्षरा, 2. नीलकण्ठ लिखित यवहारमयूख ३ वीरमित्रोदय 4. निर्णय सिन्धु 5. पराशरमाधव्य, 6 विवाद ताण्डव।
पंजाब शाखा– यह शाखा पूर्वी पंजाब वाले प्रदेश में प्रचलित है।
इस शाखा में निम्नलिखित प्रमाण मान्य है – (1) मिताक्षरा (2) वीरमित्रोदय (3) पंजाबी प्रधाएँ।
(ख) दायभाग–‘ दायभाग’ जीमूतवाहन द्वारा लिखित एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत धन्य माना जाता है। इसके रचना काल के विषय में विद्वानों के बीच काफी मतभेद हैं लेकिन समयत: यह 11वीं शताब्दी में लिखा गया। विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्रीधन पर यह एक प्रमुख धन्य माना जाता है तथा इन विषयों पर एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन करता है। इस ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जन्मतः पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है।
यह शाखा समस्त पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के प्रदेशों में प्रचलित है। निम्नलिखित ग्रन्थ इस शाखा की प्रमुख प्रमाणिक कृतियाँ हैं (1) दायभाग, (2) दायतत्व (3) दायक्रम संग्रह (4) बीरमित्रोदय, (5) दत्तक चन्द्रिका।
मिताक्षरा तथा दायभाग में अन्तर- मुख्यतः हिन्दू विधि में मिताक्षरा तथा दायभाग दो ही मुख्य शाखाएँ हैं। इन शाखाओं में अन्तर कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। इन दोनों शाखाओं में जो मौलिक अन्तर है, उसको इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है –
1. संयुक्त सम्पत्ति के विषय में – मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है जबकि दायभाग शाखा में पुत्र का पिता की सम्पत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न होता है। इसके अलावा मिताक्षरा में पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियन्त्रित होता है। एक के मरने के बाद संयुक्त परिवार का दूसरा उसके अंश को उत्तरजीविता से प्राप्त होता है। दायभाग में इसके विपरीत पिता का अपने जीवन काल में सम्पत्ति पर परम अधिकार होता है, पुत्र का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता प्रत्येक व्यक्ति का अंश उसकी मृत्यु पर दाय के रूप में उसके दायादों को प्राप्त होता है। उत्तरजीविता का नियम यहाँ लागू नहीं होता।
2. हस्तान्तरण के सम्बन्ध में – मिताक्षरा में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त सम्पत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तान्तरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त है इसके विपरीत दायभाग के अन्तर्गत संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अविभक्त सम्पत्ति में अपने अंश को हस्तान्तरित कर सकता है।
प्रश्न 3. विवाह विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा एक वैध विवाह के लिए कौन सो अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं? क्या इन शर्तों के उल्लंघन पर किसी दण्ड की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गयी है?
What new essential conditions are added for valid marriage in Hindu Marriage Act, 1955 by Hindu Laws (Amendment) Act, 1976? Is there any penalty for infringement of these conditions?
अथवा (or)
एक वैध हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है? क्या एक हिन्दू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह कर सकती है?
What are essential conditions of valid Hindu Marriage? Can a Hindu girl marry with a Muslim boy?
उत्तर- हिन्दुओं के मध्य विवाह एक संस्कार है। विवाह के बारे में हिन्दुओं में कहा जाता है कि विवाह जन्म-जन्मान्तर का बन्धन है तथा जन्म से पूर्व तय हो जाते हैं जि जन्म के बाद मूर्त स्वरूप प्रदान किया जाता है या लागू किया जाता है। हिन्दू विवाह क वर्तमान आवश्यक शर्तों को समझने के लिए हमें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के सम्बन्धित प्रावधानों का अवलोकन करना होगा। इस विषय में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 से पूर्व की स्थिति का अवलोकन भी समीचीन होगा।
हिन्दू विधि के पूर्व विवाह की स्थिति- धार्मिक हिन्दू विधि के हिन्दू विवाह के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक था –
1. पक्षकार वर तथा वधू एक ही जाति के होने चाहिए।
2. पक्षकार वर तथा वधू को सम्बन्धों या नातेदारी के प्रतिबन्धित श्रेणी से परे होना चाहिए अर्थात् यह आवश्यक था कि वर तथा वधू प्रतिबन्धित नातेदारियों को श्रेणी के अन्तर्गत न हों।
3. हिन्दू विवाह के सभी उचित समारोहों का पालन हुआ है अर्थात् हिन्दू विवाह के लिए आवश्यक सभी समारोह सम्पन्न हुए हों।
प्राचीन हिन्दू धर्म में प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबन्ध था अर्थात् निम्न जाति के पुरुष तथा उच्च जाति की महिला के मध्य विवाह पर प्रतिबन्ध था परन्तु अनुलोम विवाह की अनुमति थी अर्थात् उच्च जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की स्त्री के मध्य विवाह पर प्रतिबन्ध नहीं था।
ज्योतिशाह बनाम राजेश कुमार पाण्डेय, AIR 2000 Cal. 109 के बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जहाँ पर कोई पक्षकार अपना विवाह हिन्दू पद्धति के अन्तर्गत सम्पन्न नहीं करता अर्थात् अग्नि के सम्मुख मंत्रोच्चारण द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति एवं सप्तपदी गमन की रीति का अनुसरण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में वह विवाह अपूर्ण माना जाता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह की आवश्यक शर्तें – अब हिन्दू विवाह के लिए वैधता हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जाति या उपजातियों की एकरूपता, समानता आवश्यक नहीं है। अधिनियम सगोत्र नातेदारी के आधार पर विवाह में प्रतिबन्ध की मान्यता नहीं देता। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में वैध हिन्दू विवाह के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है जिनका निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है –
(1) एक पत्नी विवाह- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) के अनुसार एक विवाह के लिए यह प्रथम आवश्यक शर्त है कि वर या वधू को जीवित पत्नी या पति पहले से न हो। एक जीवित पत्नी के रहते हुए किसी पुरुष द्वारा किया गया दूसरा विवाह शून्य तथा अमान्य होगा। इस प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबन्ध लगाता है जो इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व अनुमत था। यह प्रावधान एक बाध्यकारी तथा आवश्यक शर्त प्रतिपादित करता है। इस प्रावधान के उल्लंघन में किये गये विवाह के पक्षकारों के लिए इस अधिनियम की धारा 17 में दण्ड का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारा 5 (1) के उल्लंघन में एक जीवित दम्पत्ति के रहते हुए किया गया विवाह न सिर्फ शून्य तथा अमान्य है अपितु ऐसा करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494, 495 के अन्तर्गत द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा।
लीला थामस बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 2000 एस० सी० 1650 के बाद में पति ने अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह सम्पन्न किया और आई० पी० सी० की धारा 494 के अन्तर्गत द्विविवाह के अपराध से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि धर्म परिवर्तन द्वारा प्रथम विवाह की उपस्थिति में किसी हिन्दू पक्षकर के द्वारा द्वितीय विवाह करना हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत होगा।
महाबीर बनाम सुकुमार तुला जोगन्द्रा, ए० आई० आर० (2013) एन० ओ० सी० 331 कर्नाटक के बाद में उच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया कि पति का दूसरी पत्नी के साथ विवाह को विधिमान्य नहीं माना जायेगा जिसने अपनी प्रथम पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त किये बिना ही दूसरा विवाह रचाया।
(2) पक्षकारों की सहमति – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (ii) के अन्तर्गत वैध विवाह की द्वितीय शर्त प्रतिपादित की गई है। इस अधिनियम को सन् 1976 में संशोधन के पश्चात् सम्पत्ति को या विवाह के पक्षकारों की सहमति को प्रधानता दी गई। इस शर्त के अनुसार –
(क) विवाह के पक्षकारों वर या वधू को विकृत चित्त के कारण सहमति देने में असक्षम नहीं होना चाहिए।
(ख) यद्यपि वर या वधू वैध सहमति देने में समक्ष तो है परन्तु इस प्रकार के रोग से इस सीमा तक ग्रसित है कि वे विवाह के अयोग्य हैं तथा सन्तान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है।
(ग) पागलपन के बार-बार दौरे वर या वधू को नहीं आने चाहिए। यदा-कदा एक आध बार दौरे आने को बार-बार दौरे की संज्ञा नहीं दी जा सकती। (या ‘मिर्गी’ शब्द सन् 1999 के संशोधन से हटा दिया गया)
(घ) जो व्यक्ति बौद्धिक शक्ति में इतना कमजोर हो कि वह सही बात न समझ सकता हो।
उपरोक्त शर्तों को बालकृष्ण बनाम लोकिमा (1984) के बाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई।
करेदला पार्थ सारथी बनाम गाँगूला रामानम्मा, ए० आई० आर० (2015) एस० सी० 891 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की अभिपुष्टि की कि जहाँ कोई स्त्री पुरुष काफी समय से पति-पत्नी की तरह रह रहे हों और समाज के लोग उन्हें पति-पत्नी समझते हों और उन्होंने अपने बीच कोई विवाह सम्पन्न न किया हो बल्कि उस स्त्री का नाम बैंक खाते व अन्य दस्तावेजों में अपने साथ पत्नी के रूप में दर्शाया हो वहाँ ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने ऐसी स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया। न्यायालय का यह मानना था कि यद्यपि ऐसे मामले में हिन्दू रीति-रिवाज का पालन नहीं किया गया था लेकिन वह मानसिक रूप से उसको पत्नी मानता था ऐसी परिस्थिति में ऐसी स्त्री को पत्नी को उपधारणा को जायेगी।
(3) विवाह की आयु (Age of marriage)- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को धारा 5 (iii) के अन्तर्गत वैध विवाह की तीसरी शर्त प्रतिपादित की गयी है। इस शर्त के अनुसार एक वैध हिन्दू विवाह के लिए यह आवश्यक है कि विवाह के समय वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष या वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु यदि 15 वर्ष से कम उम्र की वधू का विवाह सम्पन्न होता है तो यह विवाह न तो शून्य है न हो शून्यकरणीय (Voidable) परन्तु यह विवाह 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को सम्पन्न कराने वाले लोगों को दण्डित करने का प्रावधान करता है।
दुर्योधन बनाम वेन्डावती (1977) में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) के प्रतिकूल सम्पन्न विवाह अर्थात् 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष तथा 18 वर्ष से कम उम्र की वधू के मध्य सम्पन्न विवाह धारा 11 के अन्तर्गत शून्य या अमान्य नहीं होगा।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सन् 1976 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि एक लड़की, जो 15 वर्ष से ऊपर की है परन्तु 18 वर्ष से कम उम्र की है, का विवाह सम्पन्न होने पर यदि लड़की इस विवाह का खण्डन करती है तो वह विवाह को खण्डित (विघटित) कराने हेतु न्यायालय की आज्ञप्ति (decree) प्राप्त कर सकती है। यह एक वधू या लड़की को जिसका विवाह 15 वर्ष से कम की उम्र में हुआ है एक अतिरिक्त आधार देता है जिसके आधार पर वह विवाह विघटित कराने की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकती है।
परन्तु सन् 1978 के अधिनियम 2 के अनुसार वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष तथा वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी आवश्यक है।
कोकुला सुरेश बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य, ए० आई० आर० (2009) आन्ध्र प्रदेश 52 के बाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बात की सम्पुष्टि की कि यदि अवयस्क कन्या का विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (3) के उल्लंघन में सम्पन्न किया गया है वहाँ ऐसा विवाह न तो शून्य होगा और न ही शून्यकरणीय होगा और उस स्थिति में विवाहिता का पति ही नैसर्गिक संरक्षक माना जायेगा न कि उसका पिता।
(4) प्रतिबन्धित डिग्री के ऊपर विवाह होना चाहिए – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (4) चौथी तथा पाँचवी शर्त का प्रतिपादन करती है, जो निम्न है –
(1) विवाह के पक्षकार वर या वधू प्रतिबन्धित नातेदारी के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिए। परन्तु यदि उनमें प्रतिबन्धित नातेदारी में विवाह करने की प्रथा या रीति है तो यह शर्त लागू नहीं होगी। [ धारा 5 (4) ]
श्रीमती शकुन्तला देवी बनाम अमर नाथ, ए० आई० आर० 1982 पी० एण्ड एच 22 के निर्णय में पंजाब उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि धारा 5 (iv) में दी गई विवाह-वैधता की शर्त प्रधाओं के प्रमाणीकरण से बाधित है अर्थात् प्रथाओं की स्थिति में दो प्रतिषिद्ध सम्बन्धियों के बीच वैध विवाह हो सकता है। इन प्रथाओं को अति प्राचीन तथा मानव स्मृति के परे होना चाहिए।
(2) विवाह के पक्षकार वर तथा वधू सपिण्ड नहीं होने चाहिए परन्तु यदि उनके मध्य प्रचलित प्रथा या रीति-रिवाज के अनुसार सपिण्ड नातेदारियों में भी विवाह की अनुमति है तो यह शर्त लागू नहीं होगी। (धारा 5(5) ) शर्तों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था-(i) अधिनियम की धारा 5 की प्रथम शर्त के उल्लंघन होने पर दो परिणाम उत्पन्न होते हैं –
(a) धारा 11 के अनुसार विवाह अकृत एवं शून्य हो जायेगा तथा (b) धारा 17 के अनुसार जो भी पक्षकार शर्त का उल्लंघन करेगा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अनुसार दण्ड का भागी होगा।
(ii) अधिनियम की धारा 5 के द्वितीय शर्त के उल्लंघन होने पर धारा 12 (ख) के अनुसार विवाह शून्यकरणीय हो जाता है।
(iii) आयु से सम्बन्धित शर्त के उल्लंघन पर विवाह किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, किन्तु धारा 18 के अनुसार यह अपराध है। पूर्व में अपराधी पक्षकार का इसका दण्ड सादा कारावास 15 दिन तक का, अथवा 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता था। किन्तु वर्तमान में इस सम्बन्ध में सन् 2007 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 20 के द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन में यह प्रावधान दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 5 के खण्ड (3) में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन करेगा तो ऐसी शर्तों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास से अथवा एक लाख रुपये तक का जुमांना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
(iv) जो व्यक्ति धारा 5 के खण्ड (iv) एवं (v) के दिये गये उपबन्ध के प्रतिकूल विवाह करेगा- धारा 11 के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध सम्बन्धियों एवं सपिण्ड के साथ विवाह करेगा शून्य करार किया गया है तथा धारा 18 (ब) के अधीन इस प्रकार विवाह करने के दोष में दोषी पक्षकार को एक महीने का साधारण कारावास अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
अरुण लक्ष्मण राव नावलकर बनाम मीना अरुण नावलकर, ए० आई० आर० (2006) बम्बई 342 के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 5 (5) के अन्तर्गत ऐसे विवाह को मान्यता दी जा सकती है यदि विवाह के पक्षकार ऐसी किसी प्रथा से शासित होते हैं जिसके अनुसार सपिण्ड सम्बन्धियों में भी विवाह हो तो उपर्युक्त शर्त नहीं लागू होती और विवाह मान्य समझा जायेगा।”
क्या एक हिन्दू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर सकती है- नहीं, केवल तभी कर सकती है जब मुस्लिम पुरुष धर्म परिवर्तन करके हिन्दू हो जाये क्योंकि हिन्दू विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी आवश्यक है। (हिन्दू विवाह अधिo 1955 की धारा 7) तथा मुस्लिम विधि भी इसकी अनुमति नहीं देती इसमें भी ये लोग तभी वैध विवाह कर सकते हैं जब हिन्दू लड़की अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म अपना ले।
प्रश्न 4 वर्तमान हिन्दू विधि में विवाह न तो संस्कार है और न ही संविदा विवेचना कीजिए।
Discuss the marriage has not remained a sacrament marriage and has also not become contract under present Hindu law.
अथवा (or)
“हिन्दू विवाह एक संस्कार है न कि एक संविदा। विवेचना कीजिए।
A Hindu marriage is a sacrament, not a contract, discuss.
अथवा (or)
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हिन्दू विवाह की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
Analyse the nature of Hindu Marriage under the Hindu Marriage Act, 1955.
उत्तर- हिन्दू विवाह का वर्तमान स्वरूप- हिन्दू विवाह का वर्तमान स्वरूप प्राचीन स्वरूप जैसा नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण अधिनियमों का पारित होना है। सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कई अधिनियम पारित किए गए जैसे हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1956, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929, हिन्दू विवाहित नारी का पृथक आवास एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1946, हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1946, हिन्दू विवाह विधि मान्यता अधिनियम, 1949 परन्तु उपर्युक्त अधिनियमों के पारित होने के बावजूद जब अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 पारित हुआ।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का हिन्दू विवाह पर प्रभाव– यह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के पारित होने के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस अधिनियम ने विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को पूर्णरूप से परिवर्तित कर दिया है अर्थात् हिन्दू विवाह का अब वह स्वरूव नहीं रह गया है जैसा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पी० वेंकटर्मन बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1987 के मामले में बताया था कि-“नि:संदेह हिन्दू विवाह धार्मिक संस्कार है यही एक संस्कार स्त्रियों के लिए भी विहित किया है। यह एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह एक ऐसा बन्धन होता है। जो अग्नि के सामने सप्तपदी पूर्ण करने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। इसे संविदा नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविदा के लिए पक्षकारों का वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है जबकि हिन्दू विवाह के पक्षकार अवयस्क एवं विकृतचित (Unsound mind) कैसा भी हो सकता है।
परन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के पारित होने के बाद आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का हिन्दू विवाह के बारे में व्यक्त किया गया उपर्युक्त मत समीचीन नहीं लगता क्योंकि हिन्दू विवाह जो धार्मिक संस्कार माना जाता था, लगभग संविदात्मक स्वरूप का गया है। विवाह को धार्मिक बन्धन एवं जन्म जन्मान्तर का साथ माना जाता था जिसे तोड़ना पाप समझा जाता था। पुरुष चाहे जैसी पत्नी मिलती थी वह उसके साथ जीवन निर्वाह करता था और स्त्री को चाहे जैसा पति मिलता था, वह उसके साथ हँसी-खुशी जिन्दगी बिताती थी। परन्तु अधिनियम ने विवाह-विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह को शून्य कराने का वैवाहिक उपचार का उपबन्ध कर हिन्दू विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को छिन्न भिन्न कर डाला है।
2. वैवाहिक विधि पर प्रभाव- हिन्दू विवाह अधिनियम ने विवाह विधि में निम्नलिखित परिवर्तन करके प्राचीन हिन्दू विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को संविदात्मक स्वरूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है –
(i) एक विवाह को मान्यता – अधिनियम ने बहुविवाह पर रोक लगा दी है और एक विवाह को विधि मान्यता प्रदान की है। दूसरा विवाह अपराध के रूप में दण्डनीय एवं शून्य घोषित किया गया है।
(ii) विवाह-विच्छेद का उपबन्ध- अधिनियम ने विवाह के पक्षकारों को विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण आदि का उपचार प्रदान कर हिन्दू विवाह के प्राचीन स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है। (iii) अन्तर्जातीय विवाह को मानयता – अधिनियम ने अन्तर्जातीय विवाह को विधिमान्य घोषित कर दिया है यहाँ तक कि हिन्दू के अर्थ के अधीन आने वाली जातियों के बीच सम्पन्न विवाह को मान्यता प्रदान की गई है।
(iv) विवाह की शर्तों का सरलीकरण – अधिनियम के अन्तर्गत सपिण्ड के विस्तार क्षेत्र को कम करके और प्रतिषिद्ध नातेदारों को सीमित करके हिन्दू विवाह की शर्तों का सरलीकरण कर दिया गया है।
(v) नए अनुतोषों का उपबन्ध।
(vi) शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को वैधता। (vii) सगोत्र विवाह को विधिमान्यता।
(viii) विवाह-विच्छेद के बाद सन्तानों के भरण-पोषण एवं अभिरक्षा के बारें में व्यापक व्यवस्था।
क्या विवाह का आधुनिक स्वरूप संविदात्मक है? – निम्नलिखित कारणों से यह कहा जा सकता है कि विवाह का आधुनिक स्वरूप संविदात्मक हो गया है –
1. सहमति से विवाह-विच्छेद की सुविधा- यद्यपि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में ही विवाह को शून्य घोषित कराने की सुविधा प्रदान की गई थी परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद कराना आसान नहीं था। इसके अतिरिक्त विवाह विच्छेद कराना आसान नहीं था। ऐसा उपबन्ध इसलिए किया गया था कि 3 वर्ष में विवाह के पक्षकार ठीक से एक दूसरे को समझ लें, यदि कोई गलफहमी हो गई हो तो दूर कर लें। परन्तु संशोधन अधिनियम, 1976 ने यह उपबन्ध करके कि “विवाह के पक्षकार आपसी सहमति से विवाह के एक वर्ष पश्चात् विवाह-विच्छेद करवा सकते है। हिन्दू विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को चकनाचूर करके हिन्दू विवाह के स्वरूप को लगभग संविदात्मक कर दिया है।
2. न्यायिक पृथक्करण और विवाह- विच्छेद के आधारों का एकीकरण विवाह विधि अधिनियम, 1976 ने न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधारों को एक कर दिया है जिससे न्यायिक पृथक्करण की उपयोगिता समाप्त हो गई क्योंकि अब कोई पक्षकार न्यायिक पृथककरण की याचिका दायर करना इसलिए पसन्द नहीं करता क्योंकि उसे उन्हीं आधारों पर विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यायिक पृथककरण और विवाह विच्छेद के आधारों के एकीकरण के उपबन्ध ने हिन्दू विवाह के स्वरूप को संविदात्मक स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्रदान की है।
3. यौन सम्बन्धी बीमारी एवं मस्तिष्क विकृतता के आधार पर विवाह विच्छेद– पहले यौन सम्बन्धी बीमारी एवं दिमागी विकृतता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री तभी प्रस्तुत की जाती थी जब कोई पक्षकार एक निश्चित अवधि से उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त होता था। परन्तु संशोधन अधिनियम, 1976 ने अवधि सम्बन्धी शर्त समाप्त करके विवाह विच्छेद को और आसान बना दिया है।
4. जारता के आधार पर विवाह-विच्छेद- संशोधन अधिनियम, 1976 के जारता के एक हो कृत्य पर विवाह-विच्छेद को डिक्री प्रदान की जा सकती है।
5. विवाह के पक्षकारों की आयु में परिवर्तन – बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1978 ने वर और वधू की आयु सीमा बढ़ा दी है। अब विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष कर दिया गया है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अधिनियमों ने विवाह-विच्छेद को आसान बनाकर हिन्दू विवाह के उस प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप को नष्ट कर डाला है जिसे पति-पत्नी का जन्म-जन्मान्तर का कभी न समाप्त होने वाला रिश्ता माना जाता था।
अब उक्त अधिनियमों ने विवाह को संविदात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है और काफी हद तक अपने प्रयत्न में सफल भी हुए हैं परन्तु फिर भी हिन्दू विवाह को मुस्लिम विवाह की तरह संविदा नहीं कहा जा सकता। अतः हिन्दू विवाह को एक ऐसा विवाह कहा जा सकता है जो न तो पूर्णरूप से सांस्कारिक रह गया है और न ही पूर्ण रूप से संविदात्मक हो गया है।
प्रश्न 5 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह का वर्णन कीजिए। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्यकरणीय विवाह के आधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Discuss void and voidable marriage under Hindu Marriage Act, 1955. Discuss the grounds of voibable marriage under Hindu Marriage Act, 1955
उत्तर- शून्य विवाह ऐसे विवाह हैं जिन्हें विधि की दृष्टि में प्रभावहीन माना जाता है। इनका अस्तित्व विधि को दृष्टि में प्रारम्भ से ही नहीं होता। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई हिन्दू विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 में) उल्लिखित उपधारा (1) (4) तथा (5) के प्रतिकूल उनमें दी गई शर्तों के उल्लंघन में किया गया है तो वह विवाह शून्य होगा तथा विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा इस विवाह के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय इस विवाह को निरस्त करने की आज्ञप्ति (decree) द्वारा शून्य घोषित कर देगा।
इस प्रकार शून्य विवाह कोई विवाह नहीं है। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। इसे विवाह सिर्फ इसलिए कहते हैं कि विवाह के पक्षकारों ने विवाह के अनुष्ठान सम्पन्न कर लिए हैं परन्तु कोई व्यक्ति अयबाधाओं तथा या सामर्थ्यहीनता के कारण इस विवाह से पति-पत्नी की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। शुन्य विवाह, विवाह न होने के कारण किसी विधिक सम्बन्ध को जन्म नहीं देता शून्य विवाह के अन्तर्गत पक्षकार के पारस्परिक अधिकार कर्तव्य तथा दायित्व जन्म नहीं लेते। अतः यदि विवाह का पक्षकार, जो शून्य विवाह है यदि उस विवाह के अस्तित्व में रहते ही दूसरा विवाह कर लेता है तो वह द्विविवाह का दोषी नहीं होगा तथा शून्य विवाह की पत्नी को यदि कोई रखैल कहकर पुकारे तो वह मानहानि का दोषी नहीं होगा। शून्य विवाह के अन्तर्गत उत्पन्न सन्तान अब धारा 16 के कारण वैध सन्तान होती है। शून्य विवाह घोषित कराने की याचिका प्रेषित होने पर तथा डिक्री पारित होने पर कोई भी पक्षकार भरण-पोषण की माँग कर सकता है परन्तु इसका कारण यह है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में इसके लिए विशिष्ट उपबन्ध है।
शून्य विवाह को शून्य करार देने के लिए शून्य घोषित करने की डिक्री की आवश्यकता नहीं होती (लीला बनाम लक्ष्मी 1968 इलाहाबाद) जब न्यायालय यह डिक्री पारित करता है तो वह पूर्व में विद्यमान एक तथ्य की घोषणा करता है अर्थात् विवाह डिक्री द्वारा शून्य नहीं होता परन्तु वह तो पहले से ही शून्य होता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत विवाह शून्य घोषित कराने हेतु विवाह का कोई पक्षकार याचिका दायर कर सकता है। शून्य विवाह के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (1) (4) तथा (5) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में किये गये हैं जैसे –
(1) यदि विवाह के एक पक्षकार को विवाह के समय पूर्व विवाह से पति या पत्नी जीवित है। [धारा 5 (1)]]
(2) यदि विवाह के पक्षकार सम्बन्धों को प्रतिबन्धित श्रेणी में आते हैं जब तक कि किसी प्रथा, रूढ़ि जिससे विवाह के पक्षकार शासित होते हैं इस सम्बन्ध के मध्य विवाह की अनुमति न देते हो। [धारा 5 (4) ]
(3) यदि विवाह के पक्षकार आपस में सपिण्ड हो जब तक उनके रूढ़ि या रीति रिवाज इनके मध्य विवाह की अनुमति न देते हो। [धारा 5 (4) ]
यदि किसी व्यक्ति को प्रथम पत्नी उसके द्वितीय विवाह को शून्य घोषित करने के लिए, याचिका दायर करती है तो वाद इस अधिनियम से शासित नहीं होगा परन्तु विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 से शासित होगा। (हरमोहन बनाम श्रीमती कमला, ए० आई० आर० 1979 उडीसा 511)
देवकी पॉझियारा बनाम शशि भूषण नारायण आजाद, ए० आई० आर (2013) एस० सो० 346 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पति के द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसकी पत्नी पहले से विवाहित है और उसने पुनः अपना विवाह उससे सम्पन्न किया है, वहाँ ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा किया गया विवाह शून्य होगा और वह अपने पति से किसी भी प्रकार का भरण-भोषण प्राप्त करने को अधिकारी नहीं होगी।
इसी प्रकार इन्द्रा शर्मा बनाम वी० के० वी० शर्मा, ए० आई० आर० (2014) एस० सो० 309 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पति पहली पत्नी की मौजूदगी में रहते हुये किसी अन्य स्त्री से विवाह रचाया हो वहाँ एक वैध पत्नी को जो अधिकार प्राप्त है, उसे वह अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अर्थात् ऐसी स्त्री को न तो भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा और न ही उसे पति की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार होगा।
शून्यकरणीय विवाह- शून्यकरणीय विवाह एक विधिमान्य विवाह है और जब तक उसके शून्यकरणीय विवाह होने की डिक्री पारित न हो जाये वह वैध तथा मान्य विवाह रहता है। शून्यकरणीय विवाह पक्षकारों में से किसी एक की याचिका द्वारा ही निर्धारित हो सकता है। यदि इस विवाह के एक पक्षकार की मृत्यु हो जाये तो शून्यकरणीय विवाह को डिक्लो पारित नहीं हो सकती। दोनों पक्षकारों के जीवित रहने पर उनमें से कोई भी यदि उसे शून्यकरणीय घोषित करवाने के लिए कोई कार्यवाही न करे तो यह विवाह विधिमान्य हो रहेगा जब तक इस प्रकार का विवाह विघटित न हो जाय उसके अन्तर्गत विधिमान्य विवाह की सब स्थितियाँ, अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व बना रहता है। शून्यकरणीय विवाह पक्षकारों को पति-पत्नी की स्थिति तथा सन्तानों को धर्मजता प्रदान करता है।
शून्यकरणीय विवाह के आधार- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 शून्यकरणीय विवाह के चार आधार निर्धारित करती है। ये आधार उन विवाहों पर भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व सम्पन्न हों या अधिनियम पारित होने के पश्चात् सम्पन्न हों। ये आधार निम्न हैं-
(1) प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर सम्भोग न होना। (2) किसी पक्षकार (प्रत्यर्थी) का विवाह के समय –
(क) चित्तविकृति के कारण विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ होना। (ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी वह इस प्रकार या उस सीमा तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वह विवाह तथा सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य है।
(ग) उसे उन्मत्तता या मिरगी का दौरा बार-बार पड़ता है।
(3) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गर्भवती होना।
(4) अर्जदाता (याचिका करने वाले) पक्षकार की सम्पत्ति बल प्रयोग या कर्मकाण्ड की प्रकृति या प्रत्यर्थी से सम्बन्धित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा प्राप्त की गई थी।
इनमें से कुछ प्रमुख आधारों की चर्चा करना आवश्यक है-
(1) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गर्भवती होना– सुरजीत बनाम राजकुमारी (1967) के बाद में पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा कि शून्यकरणीय विवाह की शर्त पत्नी का विवाह के समय गर्भवती होना है। इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि (1) प्रतिपक्षी विवाह के समय गर्भवती थी। (2) यह कि वह याचिकाकार से नहीं परन्तु अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। (3) याचिकाकार को इस तथ्य का ज्ञान विवाह के समय नहीं था। (4) यह ज्ञात होने के पश्चात् कि पत्नी गर्भवती थी याचिकाकार ने स्वेच्छा से मैथुन नहीं किया है। यदि याचिकाकार ने प्रतिपक्षी के गर्भवती होने के ज्ञान के पश्चात् स्वेच्छा से मैथुन किया है तो इसका अर्थ होगा कि याचिकाकार ने प्रतिपक्षी के अपराध को क्षमा कर दिया है।
यदि शून्यकरणीय विवाह के लिए प्रश्नगत विवाह अधिनियम पारित होने से पूर्व किया गया है तो अधिनियम लागू होने के एक वर्ष की समयावधि के अन्दर तथा अधिनियम लागू होने के पश्चात् सम्पन्न विवाहों के मामले में विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर याचिका प्रस्तुत हो जानी चाहिए।
यह साबित करने का भार कि प्रत्यर्थी गर्भवती थी. याचिकाकार पर है।
(2) कपट तथा बल – याचिकाकार की सहमति कपटे या बल द्वारा प्राप्त की गई है। तो इसके लिए विवाह को शून्यकरणीय घोषित कराने हेतु निम्न आधारों का सहारा लिया जा सकता है- (1) याचिकाकार की अनुमति बल या कपट द्वारा प्राप्त की गई थी। (2) कपट का पता लगने पर या बल प्रयोग समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर याचिका दायर कर दी गई है। (3) याचिकाकार कपट का पता लगने पर या बल प्रयोग सम्पन्न होने के पश्चात् अपनी पत्नी के साथ इच्छा से पति की तरह नहीं रहा है या रह रही है।
सन् 1976 में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में किये गये संशोधन से पूर्व निम्न तथ्य तथा परिस्थितियाँ कपट का आधार मानी जाती थीं –
(1) रोग को छिपाना (2) धर्म या जाति को छिपाना (3) शीलभ्रष्टता को छिपाना (4) अधमंजता को छिपाना (5) प्रतिपक्षी की पहचान के बारे में कपट सदैव शून्यकरणीय विवाह का आधार माना जाता रहा है।
सन् 1976 के संशोधन द्वारा यह उपबन्ध बनाया गया कि निम्न दो स्थितियों में कपट द्वारा सहमति मानी जायेगी-
1. विवाह के अनुष्ठानों (कर्मकाण्डों) के सम्बन्ध में कपट ।
2. प्रत्यर्थी से सम्बन्धित किसी तात्विक लाभ या परिस्थिति के बारे में कपट।
इस प्रकार शून्य विवाह वह है जो विधि की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य होता है तथा इसमें विवाह के पक्षकार कोई अधिकार या दायित्व या स्थिति नहीं पाते। शून्य विवाह की डिक्री न्यायालय की एक ऐसे तथ्य की घोषणा मात्र है जो पहले विद्यमान था। यहाँ संतान वैधता तथा पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार विवाह के आधार पर नहीं अपितु अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर पाते हैं।
जबकि शून्यकरणीय विवाह जब तक याचिका देकर कुछ आधारों को साबित न कर दिया जाय तब तक वैध माने जायेंगे तथा न्याय निर्णय के पश्चात् वे असमय होते हैं। शून्यकरणीय विवाह के अन्तर्गत पक्षकारों की विधिक स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्य जन्म लेते हैं।
परमिन्दर चरण सिंह बनाम हरजीत कौर, ए० आई० आर० (2003) एस० सी० 2310 के मामले में वादी ने अपना विवाह एक तलाकशुदा स्त्री से किया। उसका यह कहना था कि उसको पत्नी के विवाह-विच्छेद का कोई ज्ञान नहीं था और इस आधार पर वह अपना विवाह अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत शून्य घोषित कराना चाहता था, लेकिन पति इस आशय का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः न्यायालय ने पति के बाद को खारिज करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि पत्नी ने कोई कपटपूर्ण आचरण एवं गलत कथन नहीं किया था। अतः ऐसी स्थिति में उस विवाह को शून्यता की आज्ञप्ति नहीं प्रदान की जायेगी।
महेन्द्र सिंह बनाम शालिनी, ए० आई० आर० (2014) आन्ध्र प्रदेश 43 के मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिगत व्यक्त किया गया कि जहाँ पति के द्वारा यह प्रकट नहीं किया गया था कि वह सिरोयसिस जैसे गम्भीर रोग से पीड़ित था, वहाँ इसे प्रकर न किये जाने आधार पर पत्नी के द्वारा विवाह को शून्य घोषित कराने की आज्ञप्ति कपट के आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पति जिस बीमारी से पीड़ित है तथा वैवाहिक सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करता।
प्रश्न 6. दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना की प्रकृति को एक वैवाहिक उपचार के रूप में समझक्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अपने मत को न्यायिक निर्णयों के प्रकाश के समझाइए।
Discuss the nature of restitution of conjugal rights as a marital remedy. Does it violate right of personal liberty Explain your view in light of judicial decisions.
उत्तर- दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन (Restitution of Conjugal Rights)– विवाह द्वारा पति-पत्नी पर एक दूसरे के साहचर्य और सहवास का दायिता उत्पन्न होता है परन्तु यदि एक पक्षकार दूसरे के साथ रहने से इन्कार करता है तो क्या दूसरा पक्षकार इन्कार करने वाले पक्षकार को अपने साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। यहूदी विधि में दाम्पत्य अधिकारों में पुनः स्थापन अर्थात् इन्कार करने वाले पक्षकार का व्यक्ति पक्षकार के साथ-साथ दाम्पत्य सम्बन्ध पुनः स्थापित करने का प्रावधान था यहूदी विधि में यह उपबन्ध अंग्रेजी विधि के माध्यम से हिन्दू विधि में भी आ गया दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिक्रो (आज्ञप्ति) का तात्पर्य है कि न्यायालय दोषी पक्षकार को निर्दोष पक्षकार के साथ रहने की आज्ञा देता है। प्रारम्भिक काल में इस आज्ञा का पालन प्रतिपक्षी को गिरफ्तारी करके याचिकाकार को सुपुर्द करके किया जाता था। इस समय यह उपचार पति को ही प्राप्त था क्योंकि पति का पत्नी का दाम्पत्य अधिकार था। कुछ समय उपरान्त यह अधिकार पत्नी को भी प्राप्त हो गया तथा दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री को प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी द्वारा प्रवर्तित कराने का उपबन्ध समाप्त कर दिया गया यद्यपि डिक्री अब भी विपक्षी की सम्पत्ति कुर्क करके लागू की जा सकती है। आधुनिक अंग्रेजी विधि में दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन के वैवाहिक उपचार को समाप्त कर दिया गया है।
भारतीय विधि के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिक्री को प्रतिपक्षी को सम्पत्ति कुर्क करके प्रवर्तित कराया जा सकता है (दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 21 नियम 32) ।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत जब पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से उचित कारण के बिना अलग कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन, अर्जी द्वारा कर सकेगा और न्यायालय इस अर्जी में किये गये कथन की सत्यता के बारे में तथा इस बारे में कि आवेदन को मंजूर न करने का कोई वैध आधार नहीं है इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर तद्नुसार अधिकारों का पुनः स्थापन डिक्री द्वारा करा सकेगा।
इस प्रकार धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों को पुनः स्थापन की डिक्री प्राप्त करने हेतु तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है –
1- यह कि प्रतिपक्षी युक्तियुक्त कारण के बिना साहचर्य से अलग हो गया है।
2- यह कि न्यायालय याचिकाकार द्वारा याचिका में कथित बयानों को सत्यता के बारे में सन्तुष्ट है।
3- यह कि अनुतोष प्रदान करने के मार्ग में कोई अन्य बाधा नहीं है।
डॉ० बिन्नी बी० बनाम जयन पी० आर०, ए० आई० आर० (2016) केरल 59 के मामले में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया कि कुर्मा सम्प्रदाय के लोग जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग में सम्मिलित किये गये हैं, जिस सम्प्रदाय में विवाह उनके प्रथा व रूदि के अन्तर्गत सम्पन्न होता हो और जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू न करने के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया हो, ऐसी स्थिति में ऐसे समुदाय के लोग हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबन्धों का लाभ नहीं ले सकते।
साहचर्य से अलग होना– साहचर्य से पृथक् होने का तात्पर्य याचिकाकार का साहचर्य बिना अनुमति या सहमति के छोड़ देना है। इस सम्बन्ध में भारतीय न्यायालयों के समक्ष एक प्रश्न यह खड़ा हुआ कि पति के आदेशानुसार पत्नी का अपनी नौकरी या कार्य को न छोड़ना क्या साहचर्य से अलग होने की कोटि में आयेगा। तीरथ कौर बनाम कबाल सिंह के बाद में पत्नी को पतिगृह से दूर एक नौकरी मिल गई। वह वहाँ रहने लगी। कभी-कभी पति भी उसके साथ जाकर रह लेता था। कुछ समय पश्चात् उनमें मन-मुटाव हो गया। पति ने पत्नी को नौकरी त्याग कर अपने पास रहने का आदेश दिया। पत्नी ने अपने लिखित कथन में कहा कि वह पति के साथ सहवास करना चाहती है परन्तु नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि संसार की किसी भी विधि के अन्तर्गत पत्नी अपने पति के साहचर्य से इस भाँति विलग नहीं हो सकती अर्थात् पति अपनी पत्नी को नौकरी त्याग कर अपने साथ रहने के लिए विवश कर सकता है।
परन्तु गया प्रसाद बनाम भगवती (1965) में इसी प्रकार के तथ्य पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि हिन्दू समाज की सामान्य मान्यताओं के अनुसार पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने दाम्पत्य उत्तरदायित्व पतिगृह में रहकर पूरे करे और वह पति से पृथक् घर बसाकर रहने की अपनी एकतरफा इच्छा को पति पर यह कह कर नहीं थोप सकती कि उसे उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि जहाँ वह नौकरी करती हो उसका पति उसके साथ आकर रहे। न्यायमूर्ति श्री भार्गव ने कहा कि पत्नी का यह आचरण अभित्यजन की संज्ञा में आता है।
परन्तु उपरोक्त निर्णय के विपरीत मत तीरथ कौर के वाद (1975) में रेवेन्यू लॉ रिपोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्त्री पुरुष के बीच नियोजन के अनुसार ही समानता के इस युग में पत्नी द्वारा नौकरी करने तथा पति के आदेश पर उसे न छोड़ने को साहचर्य से अलग हो जाना नहीं कहा जा सकता। रमेश (1972) के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति काटजू ने कहा कि पति के निर्देश पर पत्नी द्वारा अपने पद से त्याग पत्र न देना दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तथा यदि पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध भी नौकरी या अन्य कोई कार्य करे तो यह साहचर्य से विलग होना नहीं कहा जायेगा तथा दाम्पत्य अधिकारों की पुन: स्थापना का आधार नहीं बनेगा। राधाकृष्णन बनाए धनलक्ष्मी (1975) में मद्रास उच्च न्यायालय, मिजुमल बनाम देवी (1977) में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया तथा यही मत सही है।
उचित कारण क्या है, इसके विषय में कठोर सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर होगा।
क्या दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है- आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष टी० सरीधा बनाम वेंकट सुब्बैया AIR (1983) A.P. 356 में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन का अधिकार संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
डी० सरीधा बनाम सुब्बैया AIR 1983 A.P.356 के बाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन का अधिकार के उपचार घृणित, क्रूर, असभ्य, नृशंस तथा अमानवीय है तथा यह व्यक्ति के मान व मर्यादा और एकांतता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इस अनुतोष से नारी की इस स्वतंत्रता का हनन होता है कि कब किस समय तथा किस प्रकार वह गर्भ धारण करके सन्तानोत्पत्ति करना चाहेगी। पुनः स्थापन की डिक्री से राज्य उसे उसकी इच्छा के विपरीत गर्भाधान करने के लिए बाध्य करती है अतः यह उपचार असंवैधानिक है।
इसके विपरीत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवध बिहारी रोहतगी ने हरविन्दर कौर बनाम हरमन्दर सिंह चौधरी, (ए० आई० आर० 1984 दिल्ली 66) के बाद में कहा कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन का उपचार विवाह के पक्षकारों के बीच मतभेद समाप्त कर उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाता है।
सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, AIR 1984 S.C. 1562 के वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सत्यसांची मुखर्जी ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन का उपचार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि आज दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिक्री को प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता सिर्फ उसकी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है तथा यह उपचार पति तथा पत्नी को एक साथ रहने को प्रोत्साहित करता है, उनके विवाह को टूटने से रोकता है।
परन्तु यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यदि पति-पत्नी के मध्य सम्बन्ध कटुता की इस सीमा तक पहुँच चुके हों कि उन्हें पुनः स्थापित करने में किसी पक्ष को बाध्यता हो तो तनाव एवम् कटुतापूर्ण जीवन व्यतीत करने से बेहतर होगा कि उनमें सम्बन्ध विच्छेद हो जाय।
प्रश्न 7. हिन्दू विधि के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण के अधिकारों के सम्बन्ध में विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्या परिवर्तन किये गये हैं? क्या यह परिवर्तन हिन्दू समाज की आवश्यकता के अनुकूल है?
What changes have been brought by the Marriage Law (Amendments) Act, 1976 in the law relating to grounds of Judicial Separation under Hindu Law? Whether such amendments are according to the needs of the Hindu society?
उत्तर- न्यायिक पृथक्करण (Judicial separation)- वैसे तो पति-पत्नी दोनों का ही एक पवित्र कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को साहचर्य प्रदान करें परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब पति-पत्नी का एक साथ रहना सम्भव नहीं रह जाता अधिनियम की धारा 10 ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण का उपबन्ध करती है। धारा 10 यद्यपि उन आधारों को नहीं बताती जिनके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की जा सकती है परन्तु धारा 10 (1), धारा 13 में वर्णित विवाह-विच्छेद के आधारों को ही न्यायिक पृथक्करण के आधार बताती है क्योंकि विवाह विधि (संशोधन) अधिक, 1976 के अन्तर्गत त्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद के आधार एक ही हो गये हैं।
निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर पति-पत्नी कोई भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं –
(1) जारता या व्यभिचारिता का आचरण- जब किसी पक्षकार ने पति अथवा पत्नी अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से लैंगिक संभोग किया हो।
(2) क्रूरता- जब याची के प्रति दूसरे पक्षकार ने क्रूरता का व्यवहार किया हो।
(3) अभित्याग – जब दूसरे पक्षकार ने याचिका प्रस्तुत किये जाने के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष से लगातार अभित्याग किया हो।
अभित्याग के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है –
(1) बिना युक्तियुक्त कारण के अभित्याग।
(2) बिना सहमति के।
(3) याची की इच्छा के विरुद्ध।
(4) याची की स्वेच्छापूर्वक उपेक्षा के बिना।
(5) यह याचिका देने के समय से पूर्व शीघ्र व्यतीत होने वाले दो वर्ष से होना चाहिए।
जहाँ पत्नी ने पति की सहमति के बिना घर छोड़ दिया और पति दो वर्ष पूरा होने के पूर्व ही विवाह भंग करने की याचिका दायर करता है, वहाँ याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि पति ने दो वर्ष के भीतर घर लौटने का इन्तजार किये बिना ही याचिका दायर कर दी।
अध्यतम्मा भट्टर अलवर बनाम श्री देवी, ए० आई० आर० (2002) एस० सी० 89 के बाद में पति एवं पत्नी ने अपना विवाह हिन्दू रीति के अन्तर्गत किया था। विवाहोपरान्त पत्नी का आचरण पति के प्रति ठीक नहीं था, वह हमेशा पति की उपेक्षा करती थी तथा विवाह के कुछ दिनों पश्चात् वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गयी और वहाँ उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। इस दौरान पति हमेशा इस बात का प्रयास करता रहा कि वह उसके साथ रहे लेकिन पत्नी अपने पति के घर वापस नहीं लौटी तत्पश्चात् पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण का वाद दायर किया प्रस्तुत मामले में न्यायालय जे सम्प्रेक्षित किया कि पति हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पाने का अधिकारी है।
(4) धर्म परिवर्तन- जब दूसरा पक्षकार धर्म परिवर्तन के कारण हिन्दू न रह गया हो।
(5) विकृत्तचित्तता– जब दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत्तचित्त रहा हो अथवा निरन्तर या बार बार इस सीमा तक विकृतचित्त रहा हो कि आवेदक प्रत्यर्थी के साथ युक्तियुक्त रूप से नहीं रह सकता।
(6) कोढ़ (Leprosy) – स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा हिन्द विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (iv) का लोप किया गया है जिससे अब उम्र और असाध्य कुष्ठ रोग के आधार पर पक्षकारों के बीच न्यायालय के द्वारा किये जाने वाले विवाह-विच्छेद की आज्ञप्ति के आधार को समाप्त कर दिया गया है। अतः अब इस आधार पर किसी भी पक्षकार के द्वारा न्यायिक पृथक्करण की याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती।
(7) संचारी रतिजन्य रोग (Communicable Veneral Disease) – जब दूसरा पक्षकार इस प्रकार के रतिजन्य रोग से पीड़ित रहा हो जो सम्पर्क से दूसरे को भी हो सकता है।
(8) संन्यासी होना- जब दूसरे पक्षकार ने किसी धार्मिक पन्थ के अनुसार सन्यास ग्रहण कर लिया हो।
(9) सात वर्ष से लापता होना – न्यायिक पृथक्करण की डिक्री तब भी प्राप्त की जा सकती है जब विवाह का दूसरा पक्षकार सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से उन लोगों द्वारा जीवित न सुना गया हो जिन लोगों द्वारा यदि वह जीवित होता तो सुना जाता।
न्यायिक पृथक्करण का परिणाम –
न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर लेने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं –
1. सहवास के दायित्व से मुक्ति– यद्यपि न्यायिक पृथक्करण से वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त नहीं होते परन्तु याची प्रत्युत्तरदाता के साथ सहवास के दायित्व से मुक्त हो जाता है। परन्तु पक्षकार यदि चाहें तो पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं।
2. पुनर्विवाह करने पर प्रतिबन्ध- न्यायिक पृथक्करण के दौरान विवाह का कोई पक्षकार पुनर्विवाह नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ जारकर्म कर सकता है क्योंकि यदि विवाह का कोई पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के साथ जारकर्म करता है तो विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है।
3. मूल विवाह अस्तित्वहीन नहीं होता- न्यायिक पृथक्करण से विवाह का अस्तित्व अप्रभावित रहता है-यदि पक्षकार चाहें तो वे बिना पुनः विवाह संस्कार को सम्पन्न किए ही पुनः वैवाहिक जीवन प्रारम्भ कर सकते हैं।
4. एक वर्ष तक सहवास न होने पर विवाह- विच्छेद- जब न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के 1 वर्ष बाद तक विवाह के पक्षकार पुनः सहवास प्रारम्भ नहीं करते तो वह विवाह विच्छेद का आधार हो जाता है।
क्या यह परिवर्तन हिन्दू समाज की आवश्यकता के अनुकूल है?
हाँ, न्यायिक पृथक्करण में सन् 1976 में जो संशोधन किये गये, वह हिन्दू समाज की आवश्यकता के अनुकूल हैं। लेखक के अनुसार, “हिन्दू विवाह एक संस्कार होता है जिसमें विवाह का बंधन अटूट माना जाता है, बात-बात में विवाह-विच्छेद नहीं हो जाता अतः हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा न्यायिक पृथक्करण द्वारा उन्हें एक ऐसा मौका मिले ताकि वे फिर से मिल सकें इसलिए इसमें केवल वैवाहिक सम्बन्ध स्थगित रहता है टूटता नहीं और समागम के बाद पुन: पहले जैसे पति-पत्नी की अवस्था में आ जाते हैं।” अतः यह व्यवस्था लेखक के मतानुसार हिन्दू समाज के अनुकूल है।
प्रश्न 8. (i) हिन्दू विधि के अन्तर्गत न्यायालय किन आधारों पर विवाह-विच्छेद की आज्ञप्ति (डिकी) दे सकता है?
Under what grounds the Court can pass a decree of divorce under Hindu law?
(ii) विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण में अन्तर बतलाइये।
Distinguish between divorce and Judicial Separation.
उत्तर (i) – हिन्दू विवाह हिन्दुओं के प्रमुख संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। प्राचीन धर्मशास्त्र तथा प्राचीन हिन्दू मान्यताओं के अन्तर्गत हिन्दू विवाह पति-पत्नी के मध्य सात जन्मों का बन्धन माना जाता था। एक हिन्दू पत्नी अपने पति को अगले जन्म में या जन्म जन्मातर तक पति के रूप में पाने के लिए व्रत, अनुष्ठान तथा प्रार्थना करती है। इस प्रकार शास्त्रीय हिन्दू विधि के अन्तर्गत पति-पत्नी के जीवनकाल में विवाह-विच्छेद अज्ञात (अकल्पनीय) था। इसका कारण था कि हिन्दू दृष्टिकोण से विवाह एक पति तथा पत्नी के मध्य अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित करता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के द्वारा हिन्दू विवाह की विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया। इस धारा के अन्तर्गत हिन्दू विवाह पति तथा पत्नी दोनों को इस धारा में उल्लिखित आधारों में से किसी एक आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम की धारा 13 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनमें विवाह-विच्छेद (divorce) का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिनियम की धारा 14 विवाह-विच्छेद लेने के अधिकार पर कुछ समय तक सीमा अधिरोपित करती है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सन् 1976 में किये गये संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि विवाह-विच्छेद के लिए याचिका विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नहीं की जा सकती। इस सीमा के दो अपवाद हैं-(1). यदि याचिकाकर्ता को विवाह-विच्छेद प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप असाधारण कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। (2) यदि प्रत्यर्थी का असाधारण बुरा चरित्र है। इन दो अपवादित मामलों में विवाह-विच्छेद के लिए याचिका विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर भी की जा सकती
असाधारण कष्ट या असाधारण दुराचारिता क्या है, इसके बारे में हिन्दू विवाह अधिनियम मौन है। इसका अर्थ एक ऐसे कष्ट या दुराचारिता से लगाया जाना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष यदा-कदा आते हैं। यही कारण है कि इनके साथ असाधारण शब्द जोड़ा गया है। दुराचारिता में कुछ नैतिक पतन की भावना निहित है।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सन् 1976 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि किसी पति तथा पत्नी के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो गई है तब भी विवाह तभी कर सकते हैं जब- (1) विवाह-विच्छेद की डिक्की के विरुद्ध अपील करने का अधिकार न हो। (2) यदि अपील करने का अधिकार है तो अपील करने की समयावधि के अन्तर्गत अपील न की गई हो। (3) या यदि अपील की गई हो तो अपील खारिज कर दी गई हो। यह स्थापित मत है कि यदि विवाह विच्छेद के पश्चात् भी धारा 15 के उल्लंघन में विवाह किया गया है तो वह विवाह शून्य होगा। परन्तु लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण (1978) के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य न होकर अमान्य होगा। ये
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में 1976 तथा 1978 में किये गये संशोधन के पश्चात् विवाह-विच्छेद के आधार –
(1) जारकर्म- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सन् 1976 में किये गये संशोधन से पूर्व जारकर्म विवाह-विच्छेद (Divorce) का एक आधार था जारकर्म का सामान्य अर्थ है कि किसी वैध विवाह की जीवित पत्नी के रहते हुए किसी अन्य की पत्नी के साथ अवैध (अनैतिक) सम्बन्ध रखना। सन् 1976 से पूर्व जारकर्म में रहना शब्द का उल्लेख था जिसे सन् 1976 के संशोधन द्वारा स्पष्ट करने के प्रयास के फलस्वरूप अपने दम्पति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वैच्छिक संभोग पदावली, व्यभिचार में रहने की शब्दावली के साथ जोड़ी गयी।
इस प्रकार अद्यतन विधि के अनुसार यदि कोई पक्षकार वैध विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् अपने दम्पति (पति-पत्नी) के तथा पत्नी-पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से स्वैच्छिक सम्भोग करने का दोषी है तो इस व्यथित पति या पत्नी को विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय में प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
चन्द्रमोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद (1967) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जारकर्म को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। सभी मामलों में जारकर्म साबित करना होगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी पत्नी को प्रेम पत्र लिखता है जिसमें अश्लीलता है तो उसे विवाह विच्छेद का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जहाँ पुरुष एक विवाहिता स्त्री को प्रेम पत्र लिखता है इससे आवश्यक रूप में अवैध सम्बन्ध सावित नहीं हो जाता।
दीपानबिता राय बनाम रोनोब्रोतो राय, ए० आई० आर० (2015) एस० सी० 419 के बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि जहाँ पति को पत्नी के जारता का सन्देह हो और उसने एक बच्चे को जन्म दिया हो तथा बच्चे के पैतृकता सम्बन्धी विवाह विच्छेद का आधार हो वहाँ न्यायालय बच्चे के पैतृक विवाद का निर्धारण के लिये डी० एन० ए० टेस्ट कराने के लिये आदेश दे सकता है तथा पैतृकता निर्धारण के पश्चात् ही वह ऐसे मामलों में विवाह-विच्छेद की आज्ञप्ति पर निर्णय देने का अधिकार रखेगा।
श्रीमती आनन्दी देवी बनाम राजाराम, AIR 1937 Raj. 14 के बाद में पति को याचिका पर पत्नी के जारता की दोषी होने के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान कर दी गई क्योंकि पत्नी ने उस स्थिति में एक बच्चे को जन्म दिया था जबकि पति से सम्पर्क सम्भव नहीं था।
(2) अभिन्यजन तथा क्रूरता – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में सन् 1978 में हुए संशोधन से पूर्व अभिन्यजन तथा क्रूरता न्यायिक पृथककरण के लिए आधार था परन्तु 1978 में संशोधन द्वारा अभित्यजन तथा क्रूरता को विवाह विच्छेद का भी आधार मान लिया गया।
अभित्यजन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का बिना किसी उचित कारण के तथा बिना दूसरे की सहमति के स्थायी रूप में त्याग करना है। अभिव्यजन, परित्याग मात्र नहीं है परन्तु एक स्थिति का परित्याग है। परित्याग में कृत्य मात्र न होकर आचरण भी होना चाहिए। इस प्रकार यदि एक पति या पत्नी कुछ समय के लिए पृथक् रहते हैं परन्तु उनका आशय एक दूसरे का स्थायी परित्याग करके एक दूसरे के सम्बन्ध को समाप्त करना नहीं है तो उसे अभित्यजन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार यदि पत्नी पति के घर लौटना चाहती है। परन्तु पति द्वारा उसके पतिगृह को लौटने के प्रयास विफल कर दिये जाते हैं तो वह (पत्नी) अभित्यजन की दोषी नहीं है। अभित्यजन का तर्क लेने वाले पक्षकार को यह साबित करना होगा कि समस्त अभित्यजन की अवधि में प्रत्यर्थी में अभित्यजन की इच्छा विद्यमान थी।
जे० श्यामला बनाम पी० सुन्दरम कुमार, AIR 1991 NOC 29 Mad. के मामले में न्यायालय ने पत्नी को वहाँ अभित्यजन का दोषी मानने से इन्कार कर दिया जहाँ पत्नी पति से इसलिए अलग रह रही थी क्योंकि पति उस पर चरित्रहीनता का मिथ्या लांछन लगाता था।
पुनः उच्चतम न्यायालय ने के० श्रीनिवास बनाम डी० ए० दीपा, ए० आई० आर० (2013) एस० सी० 2176 के बाद में क्रूरता के दायरे को बढ़ाते हुये यह सम्प्रेक्षित किया कि जहाँ पत्नी के दुराचार के कारण पति अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है वहाँ पत्नी का यह कृत्य मानसिक क्रूरता के अन्तर्गत आयेगा, जिसके आधार पर पति विवाह-विच्छेद की आज्ञप्ति न्यायालय से प्राप्त कर सकता है।
क्रूरता को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास सन् 1897 में रसेल बनाम रसेल के बाद में किया गया। इस निर्णय के अनुसार क्रूरता ऐसा आचरण है जिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने या वैसी चोट पहुँचाने की सम्भावना है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए यह साबित करना होगा कि प्रतिपक्षी के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया गया है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में यह औचित्य पूर्ण आशंका घर कर गई है कि उसके साथ रहना हानिकारक एवम् क्षतिकर होगा। सन् 1976 के संशोधन द्वारा आशंका शब्द को समाप्त कर अब क्रूरता का व्यवहार साबित करना आवश्यक बना दिया गया है। इस प्रकार चूँकि सन् 1978 के संशोधन द्वारा क्रूरता को विवाह-विच्छेद का आधार भी बना दिया गया है अतः अब क्रूरता कोई आचरण या कृत्य या लोप है जो क्रूरता को गठित करता है, विवाह-विच्छेद का आधार होगा चाहे याचिकादाता के मन में आशंका भी उत्पन्न नहीं हो। हिन्दू विधि के अन्तर्गत क्रूरता शब्द में शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरतायें आती हैं।
ओम प्रकाश पोद्दार बनाम रीना कुमारी, ए० आई० आर० (2013) दिल्ली 209 के बाद में जहाँ यदि पत्नी का आचरण अपने पति व उसके परिवार के प्रति प्रारम्भ से ही अच्छा न हो और वह अपने पति तथा पति के माता-पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हो और जिसके आचरण की वजह से पति को अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र देना पड़ा हो और जहाँ पत्नी पति के घर बिना युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही हो, वहाँ पत्नी का यह कृत्य मानसिक क्रूरता के दायरे के अन्तर्गत आयेगा पुनः उच्चतम न्यायालय ने यह स्प किया कि जहाँ पति की किसी महिला से दोस्ती हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी पत्नी पर मानसिक क्रूरता करने का दोषी है। न्यायालय ने उपरोक्त बाद में यह स्पष्ट किया कि मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आने वाला अपराध प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भ करता है और न्यायालय को यह चाहिये कि वह ऐसे संवेदनशील मामले की गहन समीक्षा करे। [पिनाकिन महिपात्रे रावल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ए० आई० आर० (2014) एस० सी० 331]
(3) विकृतचित्तता या उन्मत्तता – वह व्यक्ति जो अपने कारोबार, कार्य व्यापार को समझने तथा चलाने में असमर्थ है या जो सामान्य आचरण करने में असमर्थ है विकृतचित्तता में जड़ता तथा पागलपन भी आता है। प्रतिपक्षी विकृतचित्त है, इसके सबूत का भार याचिकाकार पर हो।
सन् 1976 में हिन्दू विवाह अधिनिमय, 1955 में किये गये संशोधन के अनुसार अब यह साबित करना होगा कि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृतचित्त रहा है या लगातार या आन्तरिक रूप से इस किस्म से और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि याचिकाकार से प्रत्यर्थी के साथ रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। विकृतचित्तता का अर्थ मस्तिष्क के ऐसे दीर्घ स्थायी विकार या अंगशैथिल्य से है जिसके परिणामस्वरूप अन्य पक्षकार (उन्मत्त) का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गम्भीर रूप से हो जाता है। यदि विकृतचित्तता ऐसी है कि जिसके कारण याचिकाकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन्मत्त व्यक्ति के साथ रहे तो उन्मत्तता की असाध्यता या दीर्घकालीन होना ऐसी शर्त है कि दोनों मिल कर विवाह-विच्छेद हेतु क्रूरता के आधार पर आवेदन करने के आधार का गठन करते हैं।
राम रिषि बनाम सुरेश कुमारी (1985) में पंजाब उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि एक व्यक्ति को हिन्दू विधि संशोधन अधिनियम, 1976 के पूर्व इस धारा के अन्तर्गत विवाह विच्छेद का आधार मिलना चाहिए, इसी प्रकार के विचार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किरन बाला अस्थाना बनाम भैरो प्रसाद श्रीवास्तव (1982) में व्यक्त किये।
(4) कुष्ठ रोग – हिन्दू विवाह अधिनिमय, 1955 के सन् 1976 में संशोधन के पश्चात् धारा 13 (1) (4) के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के आधार पर विवाह विच्छेद प्राप्त करने हेतु दो शर्तें साबित करनी आवश्यक हैं –
(1) कुष्ठ रोग असाध्य हो। (2) कुष्ठ रोग उग्र रूप में हो।
वर्तमान में पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा कुष्ठ रोग के आधार पर पक्षकारों के बीच न्यायालय के द्वारा दिये जाने वाले विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के आधार को समाप्त कर दिया गया है। अब इस आधार पर किसी भी पक्षकार के द्वारा विवाह-विच्छेद की याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती।
(5) रतिज रोग– रतिज रोग का अर्थ संभोग के फलस्वरूप संचारी रोग है। सन् 1976 के संशोधन करने से पूर्व रतिज रोग तीन वर्ष पुराना होना आवश्यक था। अब तीन वर्ष पुरानी शब्दावली को हटा दिया गया है। अब कोई समयावधि नहीं है। सन् 1976 के संशोधन से पूर्व यह सावित करना आवश्यक था कि रतिज रोग याचिकाकर्ता से नहीं लगा है अब इन शब्दों को
सन् 1976 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि रतिज रोग याचिकाकर्ता से नहीं लगा है तथा रतिज रोग की कोई निश्चित समयावधि भी निर्धारित नहीं है। अब सिर्फ यही साबित करना पर्याप्त है कि रतिज रोग संचारी (संक्रामक) प्रकृति का है।
(6) धर्म-परिवर्तन (conversion) – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (2) के अनुसार यदि प्रतिपक्षी संपरिवर्तन (धर्म परिवर्तन) के फलस्वरूप हिन्दू नहीं रहा है तो याचिकाकार विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकता है उदाहरणार्थ एक हिन्दू सिक्ख, बौद्ध या जैन अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई, मुसलमान या पारसी या यहूदी हो जाय सम्परिवर्तन के लिए धर्म द्वारा निर्धारित अनुष्ठान का सम्पन्न करना आवश्यक है।
मदानम सीता रमतुल बनाम मदानम विमला, ए० आई० आर० (2014) (एस० ओ० सी०) 412 आन्ध्र प्रदेश के बाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि यदि विवाह का कोई पक्षकार अपने विवाह के पश्चात धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उक्त परिस्थिति में दूसरे पक्षकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।
(7) प्रवन्या ग्रहण करना या संन्यास ग्रहण करना या संसार त्यागना- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (6) के अन्तर्गत यदि एक पक्ष ने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो वह विवाह-विच्छेद की डिक्री का आधार बन सकता है।
संन्यास ग्रहण करने का अर्थ है वैवाहिक जीवन का त्याग। अत: एक अर्थ में संन्यास ग्रहण करना अभित्यजन का एक अति रूप है। अभित्यजन करने वाले से वापस आने की आशा की जा सकती है परन्तु संन्यासी से वैवाहिक जीवन में वापस आने की आशा नहीं की जा सकती है।
(8) मृत्यु की उपधारणा– विश्व की अनेक वैवाहिक विधियाँ मृत्यु की उपधारणा को विवाह-विच्छेद का आधार मानती हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) मृत्यु की उपधारणा को विवाह विच्छेद का आधार मानती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विषय में उन लोगों ने जिनको सामान्यत: उनके जीवित होने के बारे में सुना जाना चाहिए था उसके जीवित होने के बारे में पिछले सात वर्षों से कुछ नहीं सुना गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में उपधारणा कर सकता है यदि एक बार मृत्यु की उपधारणा संस्थित हो जाय तो उस व्यक्ति को व्यवहारतः मृत मान लिया जाता है तथा प्रतिपक्षी को वैवाहिक विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का आधार मिल जाता है।
हिन्दू पत्नी को विवाह-विच्छेद के अतिरिक्त या विशिष्ट आधार– हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत हिन्दू पत्नी को विवाह-विच्छेद के दो अतिरिक्त आधार उपलब्ध थे। अब सन् 1976 में इस अधिनियम के संशोधन के पश्चात् हिन्दू पत्नी को विवाह-विच्छेद के चार अतिरिक्त आधार उपलब्ध हैं –
1. अधिनियम लागू होने से पूर्व पति दूसरी बार विवाह पत्नी जीवित है। (द्विविवाह का दोषी होना)
2. विवाह होने के पश्चात् पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी है।
3. यदि हिन्दू दत्तक या भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत हिन्दू पत्नी ने पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की डिक्री प्राप्त कर ली है तथा इस डिक्री के प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष या अधिक समय तक पक्षकारों के मध्य (समागम) सम्भोग नहीं हुआ है।
4. पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ था तथा 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् तथा 18 वर्ष की आयु से पूर्व उसने विवाह का खण्डन कर लिया है। इसका कोई अर्थ नहीं कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् य पूर्व विवाह खण्डित करने के पूर्व संभोग हुआ था या नहीं।
सोनदूर गोपाल बनाम सोनदूर रजनी, ए० आई० आर० (2013) एस० सी० 2679 के बाद में पत्नी ने अपने पति पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रस्तुत किया। उपरोक्त बाद में पति अपने नौकरी की तलाश के लिये विदेश गया और विदेश में ही नौकरी के दौरान वहाँ को नागरिकता प्राप्त कर लिया, उसने अपने पत्नी को कुछ समय पृथक्करण का वाद न्यायालय में संस्थित किया। उपरोक्त बाद में पति का यह कथन था कि वह भारत के न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर है अर्थात् ऐसे मामले का विचारण भारत के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हो सकता। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पक्षकारगण के पूर्वज, कुटुम्ब मूलतः भारत के निवासी हो और वह हिन्दू विधि में शासित हो रहे हो वहाँ विवाह का कोई पक्षकार दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता बल्कि ऐसे मामले का विचारण न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अन्तर्गत कर सकता है और वहाँ न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
दोनों पक्षों (पति तथा पत्नी) की आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद- सन् 1976 के विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम के द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में धारा 13 (बी) जोड़ी गई जिसके अन्तर्गत पति तथा पत्नी आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर विवाह-विच्छेद कर सकते हैं।
इसके लिए विवाह विच्छेद की याचिका विवाह के दोनों पक्षकार साथ-साथ इस आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्हें पृथक्-पृथक् रहते एक वर्ष या अधिक का समय व्यतीत हो गया है तथा वे साथ-साथ रहने में समर्थ नहीं हैं तथा उनमें आपस में यह सहमति है कि उनके विवाह को समाप्त कर दिया जाय।
यदि यह याचिका 18 माह के पश्चात् (दाखिल करने की तिथि से) वापस नहीं ली जा जाती है तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और अपनी सन्तुष्टि के पश्चात् विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करेगा। धारा 14 के अनुसार विवाह-विच्छेद हेतु आवेदन विवाह की तिथि के एक वर्ष पश्चात् ही किया जा सकता है।
रवि बनाम शारदा (1978) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आपसी सहमति के आधार पर धारा 13 (बी) के अन्तर्गत विवाह विच्छेद प्राप्त करने हेतु धारा 13 के अन्तर्गत उल्लिखित अन्य आधारों का होना आवश्यक नहीं है।
राजेश आर नायर बनाम मीरा बाबू, ए० आई० आर० (2014) केरल 44 के बाद में केरल उच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (ब) के अधीन जहाँ कोई मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो और विचाराधीन के दौरान पक्षकारों ने पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद की याचिका यदि एक बार वापस ले ली है तो ऐसे मामले में विवाह विच्छेद का आदेश न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकेगा।
अपूर्ण मोहन घोष बनाम मानषी घोष, ए० आई० आर 1989 कलकत्ता 115 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति केवल आपसी समझौता के आधार पर नहीं ली जा सकती। जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि विवाह के पक्षकार एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और उनके सम्बन्ध इस विषम स्थिति में पहुँच चुके हैं कि साथ-साथ नहीं रह सकते, इस धारा के अन्तर्गत उपचार नहीं प्रदान किया जा सकता।
इस धारा में इन पदावलियों का प्रयोग कि वे एक वर्ष से अलग रह रहे थे और वे साथ नहीं रह सकते थे’ एक साथ किया गया समझा जाना चाहिए अर्थात् वे साथ नहीं रह सकते थे इसलिए एक वर्ष या अधिक समय से अलग रह रहे थे। उनका वैवाहिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका था, और सहवास समाप्त हो चुका था, इन बातों की अवधारणा उनके साथ न रहने की स्थिति से की जानी चाहिए तभी इस धारा के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।
श्रीमती स्वीटी ई० एम० बनाम सुनील कुमार के० बी०, ए० आई० आर० 2005 कर्नाटक के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जहाँ पति भारत के बाहर एक अच्छी सेवा में कार्यरत है और पत्नी स्वयं भी एक व्यक्तिगत कम्पनी में सेवारत थी और विवाह के पश्चात् पति-पत्नी का आपस में साथ रहना सम्भव न हो तो वह इस स्थिति में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (ब) के अन्तर्गत पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद के लिये आवेदन कर सकते हैं तथा उपरोक्त मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी एवं प्रतिवादी के आपसी विचारों को देखते हुए अपवादित स्थिति में बिना 6 माह पूर्ण हुए ही ऐसे प्रावधानों को माफ करते हुये उनको आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद करने के लिऐ आज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।
उत्तर- (ii) – विवाह-विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण में अन्तर –
न्यायिक पृथक्करण
(1) न्यायिक पृथक्करण में विवाह का अस्तित्व अप्रभावित रहता है। और पति-पत्नी के सम्बन्ध स्थगित रहते हैं, समाप्त नहीं होते।
(2) न्यायिक पृथक्करण के बाद पक्षकारों को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता अगर पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो धारा 17 के अन्तर्गत दूसरा विवाह शून्य होता है और दूसरा विवाह करने वाला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
(3) न्यायिक पृथक्करण में पक्षकारों को पुनः वैवाहिक जीवन शुरू करने का अवसर उपलब्ध होता है अर्थात् पक्षकार पुन: सहवास प्रारम्भ कर वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं।
(4) न्यायिक पृथक्करण की याचिका विवाह के बाद किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है।
विवाह-विच्छेद
(1) जबकि विवाह-विच्छेद में विवाह विघटित हो जाता है और पक्षकारों के पति-पत्नी के सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं।
(2) जबकि विवाह-विच्छेद की डिक्री के बाद पक्षकार को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। और दूसरा विवाह विधिमान्य होता है तथा पक्षकार किसी दण्ड का भागी नहीं होता।
(3) जबकि विवाह-विच्छेद में पक्षकारों को वैवाहिक जीवन शुरू करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता।
(4) विवाह-विच्छेद की याचिका कुछ असाधारण परिस्थितियों के अलावा विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 1 वर्ष पूर्व संस्थित नहीं की जा सकती।
प्रश्न 9. विवाह की अकृतता से आप क्या समझते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कौन और कब विवाह के अकृतता की डिक्री प्राप्त कर सकता है?
What do you understand by nullity of a marriage. Who and when can obtain a decree of nullity of marriage under the provisions of Hindu Marriage Act, 1955.
उत्तर- विवाह की अकृतता (Nullity of a marriage)– विवाह की अकृतता का विधिक सम्बन्ध विवाह की अड़चनों से है। यदि किसी पक्षकार में कोई अड़चन है तो वह विवाह के अयोग्य है। अवबाधा या अडचन के होते हुये विवाह करने पर विवाह विधिमान्य नहीं होगा। अधिकांश विधियों में अवबाधाओं को दो भागों में बाँटा जाता है –
(1) पूर्ण अवबाधायें (Absolute bars)
(2) वैवेकिक अवबाधायें (Discretionery bars)
पूर्ण अवबाधा के होने पर विवाह पूर्णतया अमान्य और शून्य होता है अर्थात् यह प्रारम्भ से ही शून्य माना जाता है। वैवेकिक अवबाधा के होने पर विवाह अमान्य नहीं होता है, वह शून्यकरणीय होता है, अर्थात् कोई पक्षकार चाहे तो उसका विघटन कर सकता है। कभी-कभी कुछ अवबाधाओं के होते हुए भी विवाह सम्पन्न होने पर विधि विवाह को न ही शून्य और न ही शून्यकरणीय मानती है, बल्कि उन्हें मान्यता देती है, यद्यपि पक्षकार और वैसा विवाह सम्पन्न कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करती है। विवाह की अकृतता के सन्दर्भ में विवाहों को निम्न दो प्रवर्गों में विभाजित किया जाता है –
(क) शून्य विवाह, और (ख) शून्यकरणीय विवाह
शून्य विवाह– शून्य विवाह कोई विवाह नहीं है। यह ऐसा सम्बन्ध है जो विधि के समक्ष विद्यमान है ही नहीं। इसे विवाह केवल इस कारण कहते हैं कि दो व्यक्तियों ने विवाह के अनुष्ठान सम्पन्न कर लिए हैं। परन्तु पूर्ण अवधारणाओं के होने या पूर्णतया सामध्यहीन होने के कारण कोई भी व्यक्ति पति-पत्नी की प्रास्थिति विवाह के अनुष्ठान करके ही प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ- यदि कोई भाई बहिन विवाह के अनुष्ठान सम्पन्न कर लें तो वे पति-पत्नी नहीं हो सकते हैं। धारा 11 के अन्तर्गत शून्य विवाह के निम्न तीन आधार हैं –
(क) विवाह के समय किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था। (ख) पक्षकार एक दूसरे के सपिण्ड हैं।
(ग) पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी है।
शून्यकरणीय विवाह- शून्यकरणीय विवाह एक विधिमान्य विवाह है और जब तक कि उसके शून्यकरणीय विवाह होने की डिक्री पारित न हो जाये, वह वैध और मान्य विवाह रहता है। शून्यकरणीय विवाह, विवाह के पक्षकारों में से किसी एक ही याचिका द्वारा विघटित हो सकता है।
धारा 12 शून्यकरणीय विवाह के चार आधार निर्धारित करती है-
(1) प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण
(2) प्रत्यर्थी का विवाह के समय
(i) चित्त विकृत होना
(ii) विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर
(iii) उसे उन्मत्तता का दौरा बार-बार पड़ता हो।
(3) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गर्भवती होना और
(4) कपट द्वारा सम्मति
प्रश्न 10. दत्तक ग्रहण के अर्थ की व्याख्या कीजिए। इसके उद्देश्यों एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वैध दत्तक की आवश्यकताओं की व्याख्या करें। अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से कीजिए।
Discuss the meaning of adoption mention its purposes and consequences (results). What are essentials of valid adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. Explain your answer with example.
उत्तर- दत्तक ग्रहण का अर्थ– सामान्य रूप से दत्तक का अर्थ है-दूसरे की सन्तान को अपना बना लेना। मुल्ला ने दत्तक की परिभाषा देते हुए कहा है कि दत्तक जन्म से अपरिचित एक व्यक्ति को विधिक मान्यता प्राप्त सम्बन्धीकरण प्रारूप द्वारा एक बालक के विशेषाधिकार की स्वीकृति है।
मनु के अनुसार पुरुष सन्तान की असफलता पर वैकल्पिक पुत्र ग्रहण करना ही दत्तक है। इस प्रकार दत्तक, एक परिवार से जिसमें पुत्र ने जन्म लिया है, दूसरे परिवार में उसके नैसर्गिक माता-पिता द्वारा दत्तक माता-पिता को दान के द्वारा उसके प्रत्यारोपण की क्रिया है। दत्तक को सामान्य अर्थो में गोद लेना कहते हैं। दत्तक की क्रिया के पश्चात् यह मान लिया जाता है कि दत्तक पुत्र ने नवीन परिवार में जन्म लिया है तथा उसे नवीन परिवार में अधिकारकर्त तथा एक स्थिति प्राप्त हो जाती है। दत्तक की क्रिया के पश्चात् दत्तक पुत्र अपने पुराने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है। कई विद्वानों ने कहा है कि दत्तक के पश्चात दत्तक पुत्र का (पुराने परिवार) नैसर्गिक परिवार में व्यावहारिक मृत्यु तथा दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार में विधिक जन्म होता है।
प्राचीन काल में हिन्दू विधि में पाँच प्रकार के दत्तक पुत्रों को मान्यता दी गई थी। परन्तु अब सिर्फ दत्तक तथा कृत्रिम दो प्रकार के दत्तक पुत्रों को मान्यता है। दत्तक पुत्र सम्पूर्ण भारत क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है जबकि कृत्रिम को सिर्फ मिथिला तथा आस-पास के जिलों में मान्यता प्राप्त है।
यह उल्लेखनीय है कि दत्तक को सिर्फ हिन्दू विधि में ही मान्यता प्राप्त है। मुस्लिम ईसाई, पारसी या यहूदी विधि में दत्तक को मान्यता प्राप्त नहीं है। हिन्दू विधि में भी ऐसी जातियाँ हो सकती हैं जिनमें उनकी रूढ़ि या प्रथा के अनुसार दत्तक को मान्यता नहीं दी गई हो वहाँ उनकी रूढ़ि तथा प्रथाओं को न्यायालय प्रभावी बनायेगी।
दत्तक के उद्देश्य- दत्तक का उद्देश्य दो प्रकार का है- (1) आध्यात्मिक तथा (2) अधार्मिक माता-पिता के अगले जन्म की सार्थकता के लिए पुरुष सन्तान का होना आवश्यक समझा गया है। दूसरी ओर अधार्मिक उद्देश्य के अन्तर्गत यह कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना संग पुत्र या गौण द्वारा ही हो सकती है। दत्तक का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक निरन्तरता है क्योकि शास्त्रों के अनुसार जिनके पुत्र नहीं होगा, उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार प्रत्येक हिन्दू का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह पुत्र की प्राप्ति करे। यदि वह इस कर्तव्य का निर्वाह नैसर्गिक पुत्र (संग पुत्र) को अपना करके नहीं कर सकता तो उस परिस्थिति में इस कर्तव्य की पूर्ति उसे दत्तक पुत्र के माध्यम से करनी होगी। दत्तक पुत्र अपने माता-पिता के पारिवारिक निरन्तरता को बनाये रखेगा तथा अपने मृत पूर्वजों के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठानो को पूरा करेगा। कोई भी व्यक्ति गरीब को अपना पुत्र दत्तक में नहीं देगा। परन्तु गरीबों को इच्छा भी धनिक की भाँति होती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों द्वारा दत्तक पुत्र लेने का उद्देश्य धार्मिक न होकर अपनी सुरक्षा तथा व्यवस्था का होता था।
दत्तक विधि के विभिन्न सिद्धान्तों के आधार हैं-
(1) धार्मिक (2) अधार्मिक
(1) धार्मिक सिद्धान्त के अनुसार दत्तक का उद्देश्य अपने पूर्वजों की आस्था की सन्तुष्टि के लिए धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना है। प्राचीन हिन्दू काल में हिन्दुओं के लिए पुत्र प्रत्येक पुरुष के लिए अपरिहार्य माना जाता था। इस प्रकार जिस व्यक्ति को अपना पुत्र नहीं होता था वह अपने पुत्र की धार्मिक आकांक्षा को किसी अपरिचित को अपने परिवार में पुत्र के रूप में सम्बद्ध करके पूरी करता था।
(2) अधार्मिक सिद्धान्त के अनुसार मानव स्वभाव का यह प्रमुख गुण है कि वह अपनी मृत्यु के पश्चात् भी अपनी पारिवारिक स्थिति को बनाये रखे। प्राचीन काल में परिवार में एक पुरुष का होना इसलिए भी आवश्यक होता था कि पुरुष परिवार को बाह्य खतरों से बचाने में समर्थ था। अतः पुरुष की शक्ति तथा सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परिवार में एक पुरुष का होना आवश्यक होता है।
धार्मिक सिद्धान्त के मानने वालों का तर्क था कि संस्कृत शास्त्रों के अनुसार मात्र एक पुत्र या पुत्र का पिता न होना पतित या अयोग्य होने के समान था तथा पिता को अपने श्मशान) शव से सम्बन्धित दायित्वों को पूरा करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। स: पिता के पश्चात् उसके शव से सम्बन्धित दायित्वों की पूर्ति हेतु तथा उसके परिवार में मृत्यु के पश्चात् धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वाह करने हेतु पुत्र की आवश्यकता के लिए औरस पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र अपरिहार्य हो जाता है।
अधार्मिक सिद्धान्तों के मानने वाले तर्क देते हैं कि (1) पारिवारिक रेखा को बनाये रखने के लिए औरस पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र होना आवश्यक है। (2) एक व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तथा उत्तराधिकार के लिए पृथक्-पृथक् व्यक्ति को दत्तक नहीं ले सकता। (3) अब महिलाएँ भी अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए पुत्र को गोद ले सकती हैं। (4) दत्तक उन जातियों में भी मान्यता प्राप्त है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान अज्ञात है।
परन्तु हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ने धार्मिक सिद्धान्त को निरस्त करके अधार्मिक सिद्धान्त को ही मान्यता दी है क्योंकि अब दत्तक के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अब इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी दत्तक अधार्मिक हैं तथा यदि अधिनियम की शर्तों को पूरा करते हैं जो दत्तक वैध होंगे भले ही दत्तक लेने में धार्मिक अनुष्ठान पूरे न किये गये हों।
धनराम जैन बनाम श्रीमती सूरजबाई (1973) में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में प्राचीन हिन्दू विधि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि जिन मामलों के लिए अधिनियम में प्रावधान नहीं है, उनमें प्राचीन हिन्दू विधि लागू होती है।
दत्तक ग्रहण का प्रभाव – मनु के अनुसार दत्तक द्वारा एक पुत्र को अपने पुराने परिवार से उजाड़ कर नवीन परिवार में प्रत्यारोपित किया जाता है। अतः दत्तक पुत्र अपने दत्तक पिता की सम्पत्तियों को प्राप्त करता है। वह अपने नैसर्गिक पिता की सम्पत्ति तथा नाम को कभी प्राप्त नहीं करेगा। पिण्ड में पारिवारिक नाम तथा जाति सम्मिलित हैं।
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 दत्तक के प्रभाव के बारे में निम्न प्रभावों का वर्णन करती है –
(1) दत्तक ग्रहण की तिथि से दत्तक पुत्र अपने दत्तक माता-पिता के सभी उद्देश्यों के लिए सन्तान माना जायेगा।
(2) दत्तक ग्रहण की तिथि से दत्तक पुत्र अपने दत्तक पुत्र या पुत्री के सभी सम्बन्ध अपने जन्म के परिवार से पृथक् माने जायेंगे तथा उसके सभी सम्बन्ध दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार से जुड़ जायेंगे। इस नियम के निम्न अपवाद हैं –
(क) दत्तक पुत्र अपने पुराने, नैसर्गिक परिवार में भी प्रतिबन्धित श्रेणी के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता।
(ख) यदि दत्तक क्रिया से पूर्व दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति में कोई सम्पत्ति निहित हो गई है तो वह सम्पत्ति उससे जुड़े उत्तरदायित्वों के साथ दत्तक के पश्चात् भी पूर्ववत् बनी रहेगी तथा यदि उस सम्पत्ति में स्वामित्व के साथ-साथ जन्म से परिवार के किसी व्यक्ति के भरण-पोषण का दायित्व जुड़ा है तो वह दायित्व दत्तक के पश्चात् भी बना रहेगा।
(ग) दत्तक पुत्र उस व्यक्ति को किसी अधिकार से बेदखल नहीं कर सकता, यदि वह अधिकार दत्तक की तिथि से पूर्व उस व्यक्ति में निहित हो गया है।
अर्थात् दत्तक पूर्व सम्पन्न सभी कार्यवाहियों में जिनमें अधिकार तथा दायित्व सृजित हो गये हैं, परिवर्तन नहीं कर सकता।
बामा बाई बनाम बासुदेव, (1979) में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दत्तक, दत्तक की तिथि से ही प्रभावी होता है दत्तक की तिथि से पूर्व नहीं। इस प्रकार पूर्व सम्बन्ध के सिद्धान्त को हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 12 द्वारा नकार दिया गया है।
केशर बाई बनाम करतार सिंह, (1981) में बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 द्वारा समापन कर दिया गया है। इस प्रकार एक दत्तक पुत्र अपनी दत्तक माता को उस सम्पत्ति से बेदखल नहीं कर सकता जिसकी स्वामिनी वह दत्तक ग्रहण करने की तिथि से पूर्व हो गई थी।
इस प्रकार दत्तक के अन्तर्गत एक पुत्र (सन्तान) विहीन माता-पिता किसी अन्य परिवार से एक पुत्र को उसको जन्म देने वाले माता-पिता की अनुमति से अपनी सन्तान के रूप में प्राप्त करते हैं। दत्तक का उद्देश्य माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना तथा पारिवारिक परम्पराओं को बनाये रखना है। दत्तक के परिणामस्वरूप एक दत्तक सन्तान अपने जन्म के परिवारों से सम्बन्ध विच्छेद कर नवीन परिवार में सम्बन्ध स्थापित कर लेता है।
दत्तक को हिन्दू विधि को छोड़कर अन्य विधियों में मान्यता नहीं है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में भी पुत्र को नर्क से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। मनु ने भी कहा है कि पुत्र विजय को दिलाता है, पौत्र अमरत्व प्रदान करता है तथा प्रपौत्र मोक्ष दिलाता है। धर्मशास्त्रों में भी प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य माना गया है कि वह एक पुत्र उत्पन्न करे जो उसकी मृत्यु के पश्चात् शव क्रिया अनुष्ठानों से सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करे तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक धार्मिक कर्मकाण्डों को पूरा करे क्योंकि हिन्दू धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान पुरुष द्वारा ही किया जाता है या उसमें पुरुष की प्रमुखता रहती है।
प्राचीन काल से ही औरस (सगे) पुत्र के अभाव में वैकल्पिक पुत्र प्राप्त करने की मान्यता दी गई है। महाभारत काल में भी भीष्म द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के पश्चात् उसके दो भाई विचित्रवीर्य तथा चित्रांगद शेष बचे जिसे सन्तान हो सकती थी। चित्रांगद शादी से पूर्व मर चुका था तथा विचित्रवीर्य सन्तान उत्पन्न करने में अक्षम था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् वंश आगे चलाने की समस्या का समाचान विचित्रवीर्य की पत्नियों से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुत्र प्राप्ति की अनुमति दी गई।
दत्तक भी औरस पुत्र के अभाव में पुत्र प्राप्त करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत एक पुत्र रूपी वृक्ष को दूसरे परिवार से उखाड़ कर अपने परिवार में प्रत्यारोपित किया जाता है। दत्तक के पश्चात जिसे दत्तक लिया गया है, वह अपने जन्म के परिवार से सभी सम्बन्ध तोड़ लेता है तथा नवीन दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार से सम्बन्ध जोड़ लेता है। दत्तक के उद्देश्य के लिए दो सिद्धान्त हैं –
(1) धार्मिक सिद्धान्त, (2) अधार्मिक सिद्धान्त
धार्मिक सिद्धान्त के अनुसार दत्तक का उद्देश्य अपने दत्तक पिता की मृत्यु के पश्चात् दत्तक परिवार के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना होता है तथा अधार्मिक सिद्धान्त के अनुसार दत्तक का उद्देश्य पारिवारिक श्रृंखला को कायम रखना है।
आधुनिक विधि में चूँकि पुत्री को भी दत्तक लिया जा सकता है अतः धार्मिक परिकल्पना समाप्त हो गई है।
वैध दत्तक की आवश्यकताएँ – हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 में वैध दत्तक की आवश्यकताएँ प्रतिपादित की गई हैं। धारा 6 के अनुसार किसी भी दत्तक को वैध होने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होगा –
(1) दत्तक लेने वाले व्यक्ति को दत्तक लेने का अधिकार तथा सक्षमता होनी चाहिए। [ धारा 6 (1)]
(2) दत्तक देने वाला व्यक्ति दत्तक देने में समर्थ होना चाहिए। [धारा 6 (2) ] ।
(3) जिस व्यक्ति को दत्तक लेना है वह दत्तक लिये जाने के लिए सक्षम होना चाहिए। [धारा 6 (3)]
(4) दत्तक इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन होना चाहिए। [धारा 6 (4)]
इस प्रकार दत्तक की वैधता की शर्त धारा 6 में है तथा उनका विवरण धारा 7 से 11 तक में दिया गया है, जिसका उल्लेख निम्न है –
(1) दत्तक लेने वाले व्यक्ति को दत्तक लेने का अधिकार होना चाहिए तथा वह दत्तक लेने में सक्षम होना चाहिए। [ धारा 6 (1) ] – दत्तक लेने को सक्षमता तथा अधिकार धारा 7-8 में दी गई हैं। हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के पूर्व एक स्त्री दत्तक लेने की अधिकारिणी नहीं थी तथा यदि कोई विधवा गोद (दत्तक) लेती थी तो वह अपने लिए नहीं परन्तु अपने पति के लिए गोद लेती थी। इस प्रकार वह दत्तक माता इसलिए नहीं होती थी कि उसने दत्तक लिया है परन्तु इसलिए होती थी क्योंकि वह उस व्यक्ति की पत्नी है जिसके लिए गोद (दत्तक) लिया गया था। अब हिन्दू पुरुष तथा स्त्री दोनों दत्तक लेने में समर्थ हैं। यदि-(1) वे वयस्क हैं, (2) वे स्वस्थचित्त के हैं।
पुरुष द्वारा दत्तक लेने की स्थिति में विवाहित हिन्दू अपनी पत्नी की स्वीकृति से या एक से अधिक पत्नी की दशा में सभी पत्नियों की सहमति से दत्तक ले सकता है। पत्नी की असहमति पर वह गोद नहीं ले सकता। एक अविवाहित तथा विधवा स्त्री भी गोद लेने में समर्थ है।
घीसा बाल बनाम घप्पू बाई, ए० आई० आर० (2011) एस० सी० 644 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मत की सम्पुष्टि की कि जहाँ पति के द्वारा कोई दत्तक ग्रहण किया जा रहा हो और उसकी पत्नी वहाँ पर केवल मूक दर्शक की स्थिति में हो उसने ऐसे दत्तक ग्रहण में किसी भी रूप में कोई भागीदारी न लिया हो तो उस परिस्थिति में पत्नी की सहमति, ऐसे दत्तक ग्रहण के लिये नहीं मानी जायेगी तथा पति के द्वारा लिया गया दत्तक ग्रहण ऐसी परिस्थिति में अवैध होगा।
(2) दत्तक देने वाला व्यक्ति दत्तक देने के लिए समर्थ होना चाहिए। [धारा ( 2 ) ] – धारा 9 में दत्तक देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है, इसका उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार किसी बच्चे के माता-पिता तथा संरक्षक को ही उस बच्चे को गोद देने अधिकार है अन्य को नहीं। इस प्रकार एक बालक के पिता, माता तथा संरक्षक को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को बालक को गोद देने का अधिकार नहीं है। पिता यदि जीवित हैं तो गोर (दत्तक) देने के अधिकार की उसको वरीयता होगी। परन्तु दत्तक दिये जाने वाले बालक को माता की सहमति के बिना दत्तक देने वाला पिता दत्तक नहीं दे सकता जब तक माता ने संसार त्याग कर सन्यास ग्रहण न कर लिया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न का दी गई हो।
माता को दत्तक देने का अधिकार तभी है यदि (1) पिता मर गया हो। ( 2 ) या उसने सन्यास ग्रहण कर लिया हो। (3) या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न कर दिया। गया हो।
जिस बालक के माता-पिता का पता न हो या जिसके माता-पिता मर चुके हों उसे दत्तक देने का अधिकार संरक्षक को दिया गया है परन्तु संरक्षक द्वारा दत्तक (गोद) दिये जाने के पूर्व संरक्षक के मामले में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।
(3) जिस बालक को गोद लिया जाना या दत्तक लिया जाना है वह दत्तक लिये जाने योग्य (दत्तक लिये जाने के लिए सक्षम ) होना चाहिए- हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों को दत्तक लिया जा सकता है
1. दत्तक लिये जाने वाला बालक पुत्र या पुत्री हिन्दू हो
2.उस बालक को इससे पूर्व किसी और के द्वारा गोद नहीं लिया गया हो अर्थात् एक बालक एक से अधिक बार गोद नहीं लिया जा सकता।
3. वह बालक विवाहित नहीं होना चाहिए। परन्तु यदि किसी परिवार या समाज में विवाहित बालक को गोद लेने की प्रथा है वहाँ विवाहित व्यक्ति को भी दत्तक (गोद) लिया जा सकता है।
4 – उस बालक की उम्र पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु यदि किसी परिवार में प्रथा के अनुसार 15 वर्ष से ऊपर के बालक को भी गोद लिया जा सकता है वहाँ 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को भी दत्तक लिया जा सकता है।
(4) दत्तक को वैध होने के लिए इस अधिनियम में उल्लिखित अन्य शर्तें – हिन्दु दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 निम्न शर्तों का उल्लेख करती है। जिसे वैध दत्तक के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है –
1. यदि दत्तक में पुत्र लिया जा रहा है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता को हिन्दु पुत्र या पुत्री का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र दत्तक के समय जीवित नहीं होन चाहिए (चाहे वह औरस (सगे) हो या दत्तक लिये गये हों) ।
2. यदि दत्तक में ली जाने वाली सन्तान पुत्री है तो दत्तक ग्रहण करने वाले माता या पिता को जीवित पुत्री या पुत्र की पुत्री दत्तक ग्रहण के समय नहीं होनी चाहिए (चाहे औरस या दत्तक पुत्री) ।
3. यदि दत्तक दी जाने वाली सन्तान स्त्री है तथा दत्तक लेने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक ली जाने वाली स्त्री (बालिका) तथा दत्तक लेने वाले पुरुष (पिता) की उम्र के मध्य कम से कम 21 वर्ष का अन्तर होना चाहिए।
4. यदि दत्तक किसी महिला द्वारा लिया जा रहा है तो दत्तक जिस व्यक्ति को लिया जा रहा है वह पुरुष है तो दत्तक लेने वाली स्त्री तथा दत्तक जिसे लिया जा रहा है, उस पुरुष की उम्र के मध्य कम से कम 21 वर्ष का अन्तर होना चाहिए।
5. एक ही बालक को एक साथ दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक (गोद) नहीं लिया जा सकता।
6. दत्तक देने वाले माता-पिता या संरक्षक द्वारा दत्तक दिये जाने वाले बालक को वास्तव में दत्तक दिया तथा वास्तव में दत्तक लिया जाना चाहिए अर्थात् सम्बन्धित माता-पिता या संरक्षक का यह आशय होना चाहिए कि दत्तक में बालक को जन्म के परिवार से दत्तक परिवार में स्थानान्तरित किया जा रहा है तथा उस मामले में जिसे माता-पिता का पता नहीं है, जिस संरक्षक ने उसका लालन-पालन किया है दत्तक देते समय उसका आशय पालन-पोषण वाले परिवार से दत्तक परिवार में बालक को स्थानान्तरित करने का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में दत्तक को वैध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का यह आशय रहा हो कि बालक रूपी वृक्ष को एक परिवार से उखाड़ कर दूसरे परिवार में प्रत्यारोपित किया जा रहा है अर्थात् दत्तक के पश्चात दत्तक देने वाले परिवार का आशय हो कि दत्तक पुत्र या पुत्री से उसके मूल (जन्म) परिवार से सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा।
हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 का परन्तुक इस बात को स्पष्ट करता है कि दत्तक को वैध बनाने के लिए दत्तक होम (एक अनुष्ठान) किया जाना आवश्यक शर्त नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि दत्तक की क्रिया के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठान न भी हुआ हो तो भी वह दत्तक अवैध न होकर वैध होगा।
इस प्रकार दत्तक अब एक ऐसे माता-पिता द्वारा अपनी परिवार श्रृंखला को अग्रसर करने के लिए निरन्तर बनाये रखने के लिए और पुत्र के अभाव में पुत्र की वैकल्पिक व्यवस्था है। दत्तक को वैध बनाने के लिए हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उल्लिखित आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है जिसका विस्तार धारा 7 से 11 तक में किया गया है। धारा 11 के परन्तुक का दत्तक के लिए किसी विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है।