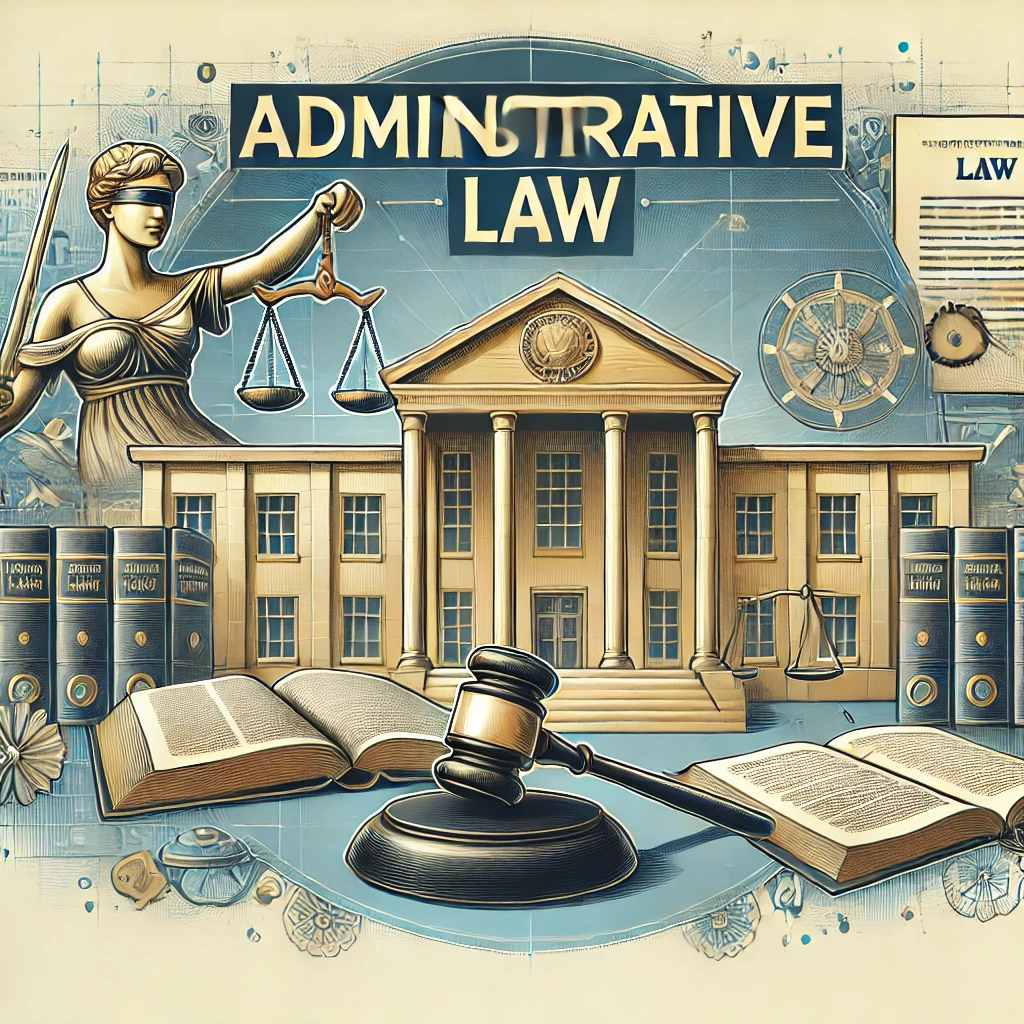Delegated Legislation in India: Concept, Need and Judicial Control
भारत में विधायी शक्ति का प्रयोग मुख्यतः संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विधायिका अपने सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकती। आधुनिक युग की जटिल समस्याओं, प्रशासनिक तंत्र की बढ़ती जिम्मेदारियों तथा समयाभाव के कारण विधायिका अनेक बार अपनी विधायी शक्ति को कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक निकायों को सौंप देती है। इसे ही अधिनियमित या प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) कहा जाता है। यह विषय भारतीय विधि-व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल प्रशासनिक दक्षता से जुड़ा है, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और विधायी उत्तरदायित्व से भी संबंधित है।
परिचय
विधान का मूल सिद्धांत यह है कि कानून बनाने का कार्य विधायिका का ही होता है। परंतु बदलते समय, बढ़ते शासन-क्षेत्र और तकनीकी-वैज्ञानिक उन्नति ने यह आवश्यक बना दिया है कि विधायिका अपनी विधायी शक्ति का कुछ अंश अन्य प्राधिकरणों को सौंपे। भारत में भी यह प्रवृत्ति तीव्र रूप से विकसित हुई है। उदाहरण के लिए – कर निर्धारण के नियम, श्रम कानूनों के अंतर्गत अधिसूचनाएँ, पर्यावरणीय नियम, तथा आपातकालीन परिस्थितियों में बनाए गए नियम और आदेश सभी प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत आते हैं।
Delegated Legislation की परिभाषा
Delegated Legislation का अर्थ है – वह विधायी शक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका, प्रशासनिक निकायों या अन्य एजेंसियों को सौंपी जाती है, ताकि वे आवश्यकतानुसार नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचनाएँ, आदेश आदि बना सकें।
सर विलियम वेड के अनुसार –
“Delegated Legislation means the exercise of legislative power by an authority other than the legislature, under the authority and control of the legislature.”
Delegated Legislation की आवश्यकता
भारत जैसे विशाल और जटिल देश में प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता अनेक कारणों से उत्पन्न हुई है:
- समयाभाव – संसद के पास सीमित समय होता है। वह प्रत्येक विषय पर विस्तार से कानून नहीं बना सकती।
- तकनीकी एवं विशेषज्ञता का प्रश्न – आधुनिक युग में कानून कई तकनीकी विषयों से जुड़ा होता है, जैसे – पर्यावरण, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा आदि। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारी ही प्रभावी नियम बना सकते हैं।
- लचीलापन और अनुकूलन – समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार नियमों में बदलाव करना आवश्यक होता है। प्रत्यायोजित विधान से यह कार्य शीघ्रता से संभव होता है।
- आपातकालीन परिस्थितियाँ – युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि के समय तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, जिसे प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- प्रशासनिक दक्षता – प्रशासनिक निकाय क्षेत्रीय परिस्थितियों को भली-भाँति समझते हैं, इसलिए वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उपनियम बना सकते हैं।
Delegated Legislation के रूप
भारत में प्रत्यायोजित विधान विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है:
- नियम (Rules) – जब कोई अधिनियम नियम बनाने की शक्ति देता है, जैसे – कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियम।
- विनियम (Regulations) – जैसे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियम।
- उपनियम (Bye-laws) – स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका या पंचायत द्वारा बनाए गए नियम।
- अधिसूचना (Notifications) – सरकार द्वारा जारी घोषणाएँ।
- आदेश (Orders) – कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश।
भारत में Delegated Legislation का संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से “Delegated Legislation” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु इसकी मान्यता अनेक प्रावधानों से मिलती है।
- अनुच्छेद 245 और 246 – विधायी शक्तियाँ संसद और राज्य विधानमंडल को प्रदान करते हैं। वे इन शक्तियों को शर्तों सहित अधीनस्थ निकायों को सौंप सकते हैं।
- अनुच्छेद 13(3) – “कानून” की परिभाषा में आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम आदि को शामिल किया गया है।
- अनुच्छेद 77 और 162 – केंद्र और राज्य की कार्यपालिका को आदेश और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 309 – केंद्र और राज्य सरकारों को सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार देता है।
भारत में Delegated Legislation पर न्यायालयों का दृष्टिकोण
भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर प्रत्यायोजित विधान की वैधता और सीमाओं पर विचार किया है।
(i) In re Delhi Laws Act, 1951
यह ऐतिहासिक निर्णय प्रत्यायोजित विधान पर मार्गदर्शक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा –
- संसद अपनी विधायी शक्ति को पूर्ण रूप से अन्य निकायों को नहीं सौंप सकती।
- परंतु संसद आवश्यक नीतियाँ निर्धारित कर सकती है और उसके कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति अन्य निकायों को दे सकती है।
- विधायिका को “आवश्यक नीति” (Essential Legislative Function) स्वयं निर्धारित करनी होगी।
(ii) Ajoy Kumar Banerjee v. Union of India (1984)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं, तो नियम बनाने की शक्ति वैध है।
(iii) Vasu Dev Singh v. Union of India (2006)
न्यायालय ने माना कि कार्यपालिका को दिए गए अधिकार “न्यायिक समीक्षा” (Judicial Review) के अधीन होंगे।
Delegated Legislation पर नियंत्रण
प्रत्यायोजित विधान की बढ़ती प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि विधायिका का अधिकार सुरक्षित रहे और नागरिक अधिकारों का हनन न हो। भारत में इस पर तीन प्रकार के नियंत्रण पाए जाते हैं:
1. विधायी नियंत्रण (Legislative Control)
- संसद अधिनियम में यह प्रावधान करती है कि नियमों को संसद के पटल पर रखा जाएगा।
- संसद नियमों को निरस्त या संशोधित कर सकती है।
- समिति प्रणाली के माध्यम से भी नियंत्रण किया जाता है, जैसे – Committee on Subordinate Legislation।
2. न्यायिक नियंत्रण (Judicial Control)
न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि –
- नियम संविधान के अनुरूप हों।
- नियम “Essential Legislative Function” का उल्लंघन न करें।
- नियम मनमाने या अलौकिक न हों।
3. सार्वजनिक नियंत्रण (Public Control)
- सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के माध्यम से नागरिक नियमों की पारदर्शिता की जाँच कर सकते हैं।
- मीडिया और जनमत भी इस पर निगरानी रखते हैं।
Delegated Legislation की आलोचना
यद्यपि प्रत्यायोजित विधान कई दृष्टियों से उपयोगी है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएँ भी की जाती हैं:
- लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत – विधायी शक्ति का प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, न कि नौकरशाही द्वारा।
- उत्तरदायित्व में कमी – कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता।
- दुरुपयोग की संभावना – कभी-कभी सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है, जैसे – असंवैधानिक आपातकालीन आदेश।
- जटिलता और भ्रम – विभिन्न नियम, अधिसूचनाएँ और उपनियम कानूनी व्यवस्था को जटिल बना देते हैं।
Delegated Legislation के लाभ
- समय और संसाधनों की बचत – संसद को छोटे-छोटे विषयों पर समय नष्ट नहीं करना पड़ता।
- विशेषज्ञता का उपयोग – तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ अधिकारियों का ज्ञान कार्य आता है।
- लचीलापन और अनुकूलता – नियमों में समय-समय पर संशोधन करना आसान होता है।
- आपातकालीन स्थितियों में उपयोगी – तुरंत आवश्यक कानून बनाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
भारत में Delegated Legislation एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। आधुनिक राज्य के विशाल कार्यक्षेत्र, प्रशासनिक जटिलताओं और त्वरित निर्णय की जरूरत ने इसे और भी प्रासंगिक बना दिया है। यद्यपि इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु विधायी, न्यायिक और सार्वजनिक नियंत्रण के माध्यम से इसे संतुलित और लोकतांत्रिक बनाए रखा जा सकता है।
इस प्रकार, प्रत्यायोजित विधान को न तो पूर्णतः अस्वीकार किया जा सकता है और न ही इसे बिना नियंत्रण के छोड़ा जा सकता है। न्यायालयों और संसद की भूमिका यही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्यायोजित विधान जनता के हितों, संविधान के मूल्यों और विधायी उत्तरदायित्व की सीमाओं के भीतर ही रहे।