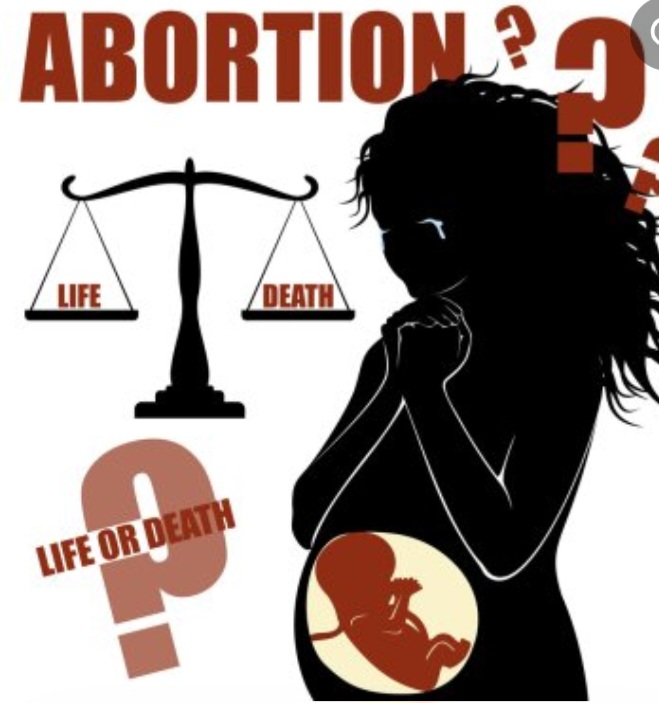गर्भपात और असमानता: शहरी बनाम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य
भूमिका
गर्भपात (Abortion) केवल एक चिकित्सीय या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक असमानताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में गर्भपात कानूनों में समय-समय पर सुधार हुए हैं, विशेषकर Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 और इसके संशोधनों के माध्यम से, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की सुविधा मिल सके। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में भारी अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर न केवल स्वास्थ्य संरचना की कमी के कारण है, बल्कि सामाजिक मानसिकता, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और जागरूकता में असमानता का भी परिणाम है।
1. कानूनी परिप्रेक्ष्य और गर्भपात का अधिकार
भारत में MTP Act के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति है, जैसे—
- गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होना
- भ्रूण में गंभीर विकृति होना
- बलात्कार या अनैतिक संबंध से गर्भधारण
- महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव
शहरी क्षेत्रों में महिलाएं इन कानूनी प्रावधानों के बारे में अपेक्षाकृत अधिक जानती हैं, और वहां चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी बेहतर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, कानून की जानकारी सीमित है और सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी आम है।
2. शहरी बनाम ग्रामीण – स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतर
(क) शहरी परिदृश्य
- शहरों में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल, क्लिनिक और NGO द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में MTP सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
- अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं अपेक्षाकृत सुलभ हैं।
- महिला डॉक्टरों और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संख्या अधिक होती है, जिससे महिलाएं अधिक सहज महसूस करती हैं।
(ख) ग्रामीण परिदृश्य
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अक्सर गर्भपात की सुविधा या प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं होते।
- दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कमी के कारण कई बार महिलाओं को शहर जाना पड़ता है।
- अनपढ़ी या कम शिक्षित महिलाओं को गर्भपात के कानूनी और चिकित्सीय पहलुओं की जानकारी नहीं होती, जिससे वे असुरक्षित विकल्प चुन लेती हैं।
3. सामाजिक दृष्टिकोण और कलंक
शहरी क्षेत्रों में गर्भपात पर खुलकर चर्चा होने लगी है, खासकर शिक्षित वर्ग में। वहां अविवाहित महिलाओं या यौन हिंसा की शिकार पीड़िताओं को कुछ हद तक सामाजिक सहयोग मिल सकता है।
वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भपात को “पाप” या “परिवार की बदनामी” समझा जाता है। वहां महिलाएं अक्सर गुप्त रूप से, असुरक्षित तरीकों से गर्भपात करवाती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन दोनों खतरे में पड़ते हैं।
4. आर्थिक असमानता का प्रभाव
शहरों में प्राइवेट अस्पताल महंगे होते हैं, लेकिन उच्च आय वर्ग की महिलाएं वहां सुरक्षित सेवाएं ले सकती हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाएं महंगे निजी इलाज का खर्च नहीं उठा पातीं, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की कमी के कारण वे झोलाछाप डॉक्टरों या बिना प्रशिक्षित दाइयों के पास जाने को मजबूर होती हैं।
यह स्थिति ग्रामीण गरीब महिलाओं को Unsafe Abortion के खतरे में डालती है, जो मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) का एक बड़ा कारण है।
5. शिक्षा और जागरूकता का अंतर
शहरी क्षेत्रों में सेक्स एजुकेशन, प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और सोशल मीडिया के कारण महिलाएं अपने प्रजनन अधिकारों के बारे में अधिक जानकार हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण महिलाओं को गर्भनिरोधक साधनों, सुरक्षित गर्भपात प्रक्रियाओं और कानूनी अधिकारों की जानकारी बहुत सीमित होती है।
6. डिजिटल और तकनीकी पहुंच का अंतर
शहरों में महिलाएं ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल, टेलीमेडिसिन और हेल्पलाइन के जरिए जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, स्मार्टफोन का सीमित उपयोग और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ये सुविधाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं।
7. कानूनी पहुंच में असमानता
शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कोर्ट, वकील और NGO के माध्यम से कानूनी मदद आसानी से पा सकती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता सेवाएं सीमित हैं और वहां महिलाओं को यह भी नहीं पता होता कि यदि डॉक्टर गर्भपात से मना कर दे तो वे शिकायत या अपील कहां कर सकती हैं।
8. सुधार और नीतिगत पहल
शहरी और ग्रामीण गर्भपात सेवाओं के बीच असमानता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव—
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण – प्रत्येक PHC और CHC में प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ और सुरक्षित MTP किट उपलब्ध कराई जाए।
- जागरूकता अभियान – गांवों में महिला समूहों, आंगनबाड़ी और ASHA कार्यकर्ताओं के माध्यम से कानूनी अधिकार और सुरक्षित गर्भपात की जानकारी दी जाए।
- मोबाइल हेल्थ यूनिट – दूरस्थ इलाकों में मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए गर्भपात सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
- डिजिटल हेल्पलाइन – टोल-फ्री नंबर और व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए ग्रामीण महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय मार्गदर्शन दिया जाए।
- NGO और सरकार का सहयोग – गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।
निष्कर्ष
गर्भपात कानून का उद्देश्य महिलाओं को उनके प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच में असमानता बनी रहती है, तो यह अधिकार केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। सुरक्षित गर्भपात केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का सवाल है। इसलिए, नीति निर्माताओं और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि चाहे महिला शहर में हो या गांव में, उसकी पहुंच समान रूप से सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक हो।