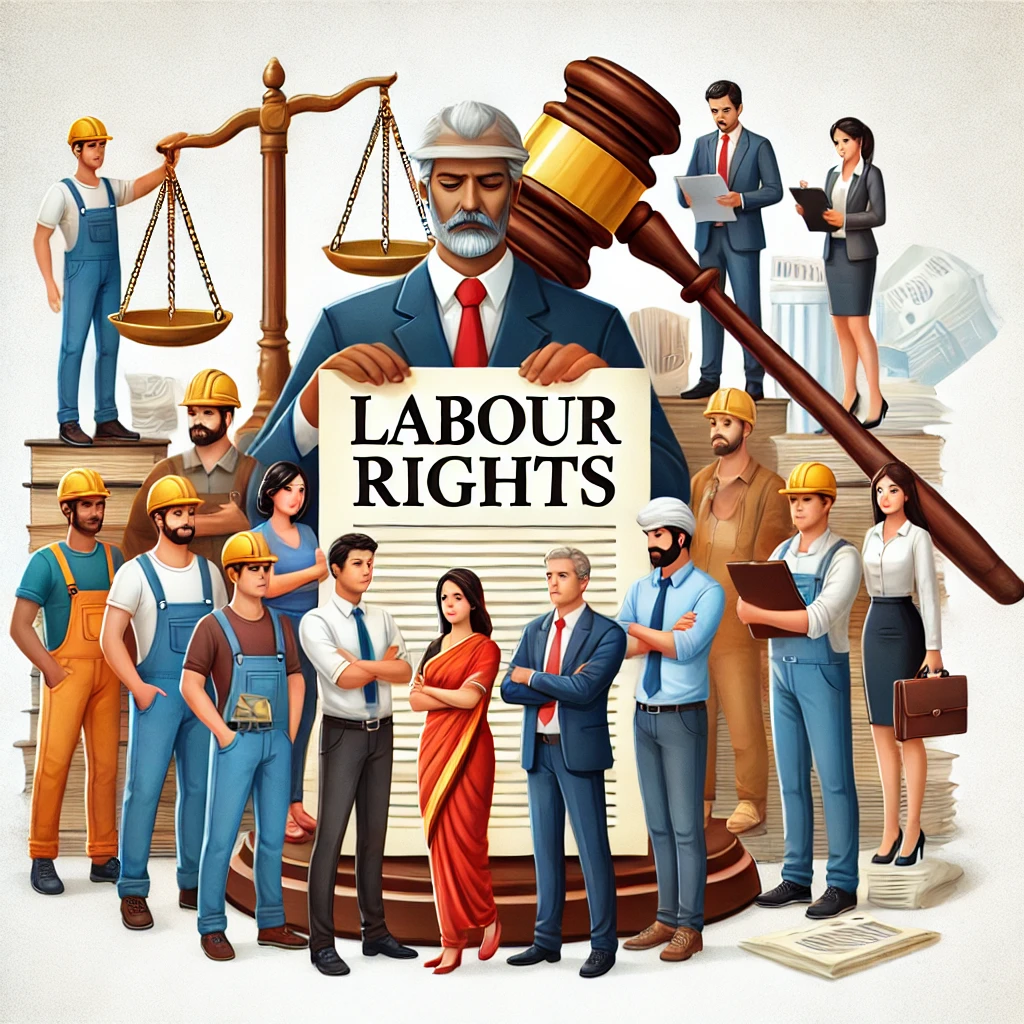मनरेगा और मज़दूर अधिकारः ग्रामीण भारत के लिए कानूनी सुरक्षा
परिचय
भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ आजीविका के प्रमुख साधन कृषि, पशुपालन और दिहाड़ी श्रम हैं। गरीबी, बेरोजगारी और मौसमी आय की अनिश्चितता ने गाँवों के लोगों को आर्थिक रूप से बेहद असुरक्षित बना दिया है। इसी सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को वर्ष 2005 में लागू किया गया।
मनरेगा (MGNREGA) न केवल एक रोज़गार गारंटी योजना है, बल्कि यह ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक कानूनी अधिकार भी सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में पहली बार ऐसा कानून बना, जो गरीबों को न्यूनतम रोजगार पाने का संवैधानिक आश्वासन देता है।
इस लेख में हम मनरेगा की मूल अवधारणा, इसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार, क्रियान्वयन की चुनौतियाँ, और इसका ग्रामीण भारत में मज़दूरों के लिए कानूनी सुरक्षा के रूप में महत्व विस्तार से समझेंगे।
1. मनरेगा क्या है?
पूरा नाम:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)
लागू वर्ष:
2005
उद्देश्य:
- ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना।
- भूख, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना।
- टिकाऊ परिसंपत्तियाँ (durable assets) जैसे कि जल संरक्षण, सड़क निर्माण आदि तैयार करना।
विशेषता:
मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून (Right-based Law) है, अर्थात् सरकार पर यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्य प्रदान करे।
2. मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार
1. रोजगार की गारंटी:
हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार मिलना उसका कानूनी अधिकार है।
2. 15 दिन में रोजगार या बेरोजगारी भत्ता:
काम की माँग करने के 15 दिन के भीतर यदि रोजगार नहीं दिया जाता तो श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) मिलना चाहिए।
3. समय पर भुगतान का अधिकार:
काम पूरा करने के 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। देरी होने पर मुआवज़ा (compensation) देना सरकार की ज़िम्मेदारी है।
4. स्थानीय कार्य:
कार्यस्थल श्रमिक के गाँव से 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। इससे अधिक दूरी पर काम देने पर परिवहन भत्ता और अतिरिक्त मजदूरी देनी होती है।
5. महिला सशक्तिकरण:
मनरेगा के तहत कम से कम 33% महिला श्रमिकों को रोजगार देना अनिवार्य है। कई राज्यों में यह प्रतिशत अधिक है।
6. काम की प्रकृति:
काम शारीरिक श्रम आधारित होता है — जैसे नहर खोदना, तालाब बनाना, सड़क निर्माण, पौधारोपण आदि। यह काम स्थायी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण में सहायक होता है।
7. पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण:
- कार्य स्थलों पर मास्टर रोल सार्वजनिक होना चाहिए।
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) के माध्यम से काम की निगरानी और भ्रष्टाचार नियंत्रण की व्यवस्था है।
3. मनरेगा के तहत आवेदन और प्रक्रिया
1. जॉब कार्ड (Job Card):
रोज़गार पाने के लिए ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य है। इसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की जानकारी रहती है।
2. रोजगार की मांग:
श्रमिक को ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से काम की माँग करनी होती है।
3. कार्य आवंटन:
काम माँगने के 15 दिन के भीतर कार्य आवंटित किया जाना चाहिए।
4. मनरेगा का महत्व: ग्रामीण भारत के लिए क्यों ज़रूरी है?
| क्षेत्र | प्रभाव |
|---|---|
| आर्थिक सुरक्षा | बेरोजगार ग्रामीणों को आय का साधन |
| मौसमी बेरोजगारी में सहारा | खेती के बाहर के मौसम में काम |
| प्रवासन में कमी | गाँव में ही रोजगार मिलने से शहरों की ओर पलायन घटता है |
| महिला भागीदारी | महिलाओं को स्वावलंबी बनाता है |
| परिसंपत्तियों का निर्माण | जल संरक्षण, सड़क, खेत तालाब जैसी संपत्तियाँ बनती हैं |
| सामाजिक न्याय | हाशिए पर खड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाना |
5. मनरेगा और कानूनी सुरक्षा
मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, यह एक कानूनी गारंटी है, जो निम्नलिखित कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है:
1. संविधान के अनुरूप:
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 39 (समान वेतन, कार्य के अवसर) जैसे प्रावधानों का व्यावहारिक रूप।
2. उत्तरदायित्व तय करता है:
- पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय है।
- समय पर भुगतान नहीं होने पर सरकारी अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रावधान है।
3. सूचना का अधिकार (RTI):
श्रमिक मनरेगा के तहत हुए काम, भुगतान, उपस्थिति आदि की जानकारी RTI के माध्यम से ले सकते हैं।
4. सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार:
हर गाँव में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया जाता है, जहाँ श्रमिक खुलकर अपनी शिकायतें रख सकते हैं।
6. मनरेगा से जुड़ी चुनौतियाँ
1. बजट में कटौती:
पिछले वर्षों में मनरेगा का बजट अपेक्षाकृत कम हुआ है, जिससे श्रमिकों को पूरे 100 दिन काम नहीं मिल पाता।
2. भुगतान में देरी:
कई राज्यों में मजदूरी का भुगतान कई हफ्तों तक नहीं होता, जिससे श्रमिकों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है।
3. जॉब कार्ड में हेराफेरी:
कई जगहों पर गरीब मजदूरों के नाम पर फर्जी कार्ड बनाकर भुगतान कर लिया जाता है।
4. काम का अभाव:
कई ग्राम पंचायतों में योजना तो है लेकिन कार्य की योजना और प्रबंधन नहीं होने से रोजगार नहीं मिल पाता।
7. समाधान और सुधार के उपाय
- मनरेगा के लिए स्थायी और पर्याप्त बजट सुनिश्चित किया जाए।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाकर समय पर मजदूरी सुनिश्चित हो।
- स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई और ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाए।
- श्रमिकों को जागरूक किया जाए कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।
- सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य और निष्पक्ष बनाया जाए।
8. केस स्टडी: मनरेगा से बदली एक गाँव की तस्वीर
राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गाँव में वर्षों से सूखा और बेरोजगारी सामान्य बात थी। मनरेगा के अंतर्गत वहाँ एक तालाब की खुदाई करवाई गई। इस काम में गाँव के लगभग 80 परिवारों को काम मिला। न केवल उन्हें आय का साधन मिला, बल्कि उस तालाब से जल संरक्षण हुआ, जिससे गाँव की खेती भी सुधर गई। यही मनरेगा की सफलता है — मजदूर को काम और गाँव को विकास।
निष्कर्ष
मनरेगा भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा कानून है जो गरीब, दलित, महिला और बेरोजगार ग्रामीणों को “काम के अधिकार” के माध्यम से गरिमा से जीने का अवसर देता है। यह कानून केवल गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है।
हालाँकि चुनौतियाँ हैं, लेकिन यदि इसे ईमानदारी, पारदर्शिता और सहभागिता से लागू किया जाए, तो यह भारत के लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन को बदल सकता है। मज़दूरों को चाहिए कि वे इस कानून के तहत अपने अधिकारों की जानकारी रखें, जॉब कार्ड बनवाएँ और कार्य की मांग करें। जागरूक मज़दूर ही अपने अधिकारों का रक्षक होता है।