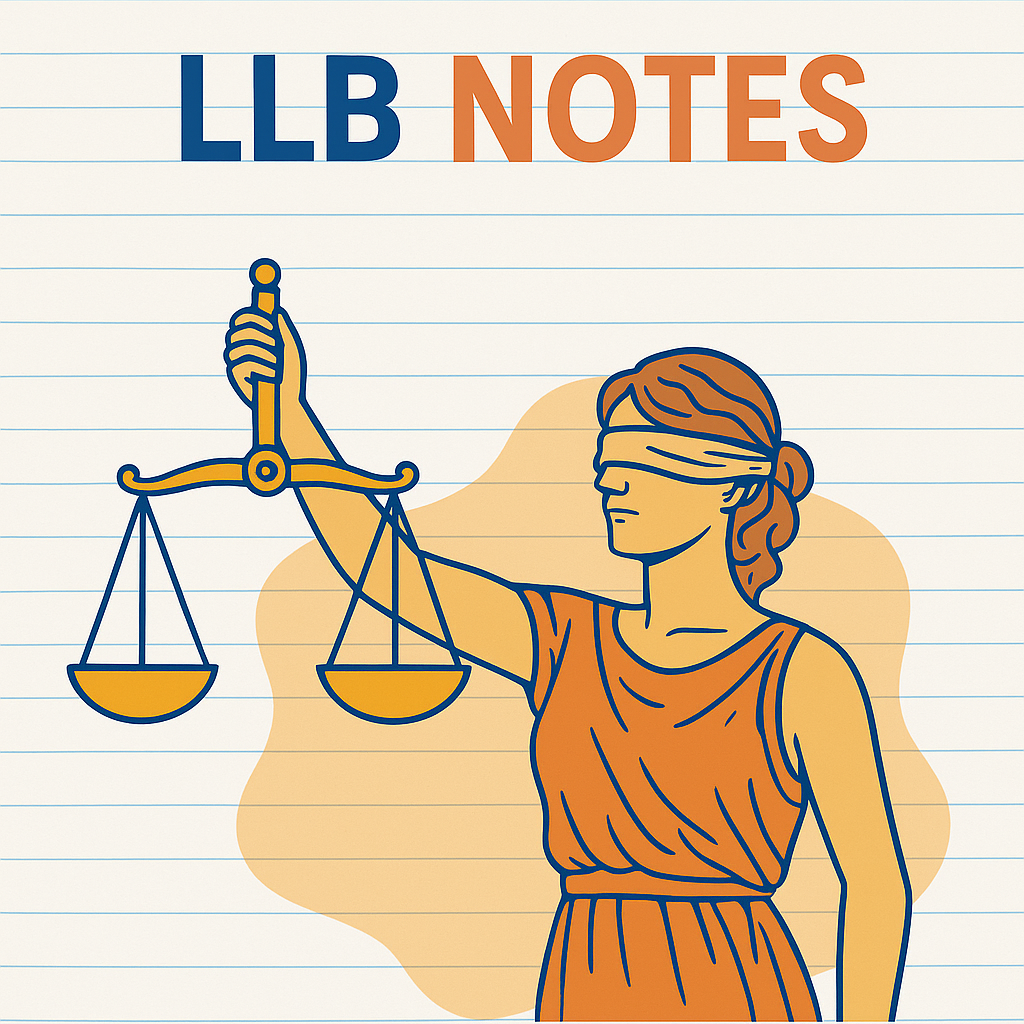भारतीय दण्ड संहिता में ‘दंड’ (Punishment) – सिद्धांत, प्रकार, औचित्य एवं आधुनिक सुधारात्मक दृष्टिकोण
1. प्रस्तावना
दंड (Punishment) आपराधिक न्याय प्रणाली का वह अंग है जिसका उद्देश्य अपराधियों को उनके अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराना, समाज में अनुशासन बनाए रखना और अपराध की पुनरावृत्ति रोकना है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (Indian Penal Code – IPC) में दंड के सिद्धांत, प्रकार और प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख है। IPC की धारा 53 में दंड के प्रकार और अन्य धाराओं में उनके लागू होने की परिस्थितियाँ निर्धारित हैं। आधुनिक समय में दंड केवल प्रतिशोध का माध्यम नहीं, बल्कि अपराधी के सुधार और पुनर्वास का साधन भी है।
2. दंड के सिद्धांत (Theories of Punishment)
दंड का औचित्य समझने के लिए विभिन्न दंड सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं –
(A) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत (Retributive Theory)
- उद्देश्य – “जैसा अपराध, वैसा दंड” (An eye for an eye)।
- अपराध को नैतिक रूप से गलत मानकर, दंड को अपराधी के लिए पीड़ा का साधन माना जाता है।
- आलोचना – यह सिद्धांत कठोर और अमानवीय माना जाता है; सुधार की संभावना को नज़रअंदाज़ करता है।
(B) प्रतिषेधात्मक सिद्धांत (Deterrent Theory)
- उद्देश्य – अपराधी और समाज के अन्य लोगों को भविष्य में अपराध करने से रोकना।
- कठोर दंड का भय उत्पन्न कर अपराध की प्रवृत्ति को समाप्त करना।
- उदाहरण – मृत्युदंड, दीर्घकालिक कारावास।
- आलोचना – केवल भय पर आधारित, सुधार की संभावना कम।
(C) निवारक सिद्धांत (Preventive Theory)
- उद्देश्य – अपराधी को समाज से अलग कर देना ताकि वह अपराध न कर सके।
- माध्यम – कारावास, निर्वासन, निरोधात्मक बंदी।
- आलोचना – अस्थायी समाधान; अपराधी के पुनर्वास की गारंटी नहीं।
(D) सुधारात्मक सिद्धांत (Reformative Theory)
- उद्देश्य – अपराधी का पुनर्वास और समाज में पुन: समावेश।
- अपराध के पीछे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को दूर करना।
- उदाहरण – शिक्षा, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खुली जेलें।
- विशेषता – आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में इसे अधिक महत्व दिया जा रहा है।
(E) प्रतिपूरक सिद्धांत (Compensatory Theory)
- उद्देश्य – अपराध से पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान करना।
- उदाहरण – जुर्माना, मुआवज़ा योजना।
3. भारतीय दण्ड संहिता में दंड के प्रकार (Section 53 IPC)
धारा 53 के अनुसार IPC में दंड के प्रकार निम्न हैं –
(1) मृत्युदंड (Death Penalty)
- अत्यंत गंभीर अपराधों (जैसे हत्या, आतंकवाद, बलात्कार के कुछ मामले) में लागू।
- IPC की धारा 302 (हत्या), 121 (देशद्रोह), 376AB (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार) आदि में प्रावधान।
- औचित्य – अत्यंत जघन्य अपराधों के लिए समाज की रक्षा और प्रतिषेधात्मक प्रभाव।
- न्यायिक दृष्टांत – Bachan Singh v. State of Punjab (1980) – मृत्युदंड केवल “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” मामलों में।
(2) आजीवन कारावास (Imprisonment for Life)
- दोषी को जीवनभर के लिए जेल में रखना, हालांकि छूट या पैरोल संभव।
- IPC की धारा 302, 376A आदि में प्रावधान।
- औचित्य – गंभीर अपराधों में अपराधी को स्थायी रूप से समाज से अलग करना।
(3) कारावास (Imprisonment)
- कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) – जिसमें श्रम कराया जाता है।
- सरल कारावास (Simple Imprisonment) – जिसमें केवल हिरासत में रखा जाता है।
- औचित्य – मध्यम स्तर के अपराधों में दंड और सुधार का संतुलन।
(4) जुर्माना (Fine)
- धनराशि के रूप में दंड, स्वतंत्र रूप से या कारावास के साथ लगाया जा सकता है।
- औचित्य – आर्थिक दंड से अपराध की लागत बढ़ाना, राज्य को राजस्व और पीड़ित को मुआवज़ा।
(5) संपत्ति की जब्ती (Forfeiture of Property)
- देशद्रोह जैसे अपराधों में (धारा 126, 127 IPC)।
- औचित्य – अपराध से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त कर अपराधी को आर्थिक रूप से दंडित करना।
4. दंड का औचित्य
दंड की आवश्यकता के पीछे मुख्य उद्देश्य –
- सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना।
- अपराध की पुनरावृत्ति रोकना।
- न्याय की स्थापना और पीड़ित को संतोष।
- अपराधियों का सुधार और पुनर्वास।
5. आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारात्मक दृष्टिकोण
आज का दृष्टिकोण यह मानता है कि –
- हर अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होता; सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण अपराध को बढ़ावा देते हैं।
- कठोर दंड हमेशा अपराध रोकने में सक्षम नहीं होते; बल्कि अपराधी और समाज के बीच दूरी बढ़ा सकते हैं।
- अपराधी के सुधार से समाज को दीर्घकालिक लाभ मिलता है।
सुधारात्मक उपाय:
- शिक्षा और प्रशिक्षण – कैदियों को साक्षर बनाना और व्यावसायिक कौशल देना।
- परामर्श और मनोचिकित्सा – मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान।
- खुली जेलें (Open Prisons) – अनुशासनप्रिय कैदियों को अधिक स्वतंत्रता।
- परोल और प्रोबेशन – अच्छा आचरण दिखाने पर समय से पूर्व रिहाई।
- पुनर्वास योजनाएँ – रिहाई के बाद समाज में पुन: स्थापन।
न्यायिक दृष्टांत:
- Mohd. Giasuddin v. State of A.P. (1977) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधारात्मक दृष्टिकोण अपराधी के मानवीय अधिकारों के अनुरूप है।
- State of Gujarat v. Hon’ble High Court of Gujarat (1998) – जेलों में सुधार और कैदियों के पुनर्वास की आवश्यकता पर बल।
6. निष्कर्ष
भारतीय दण्ड संहिता में दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि समाज की रक्षा और अपराधी का सुधार भी है। IPC ने मृत्युदंड से लेकर जुर्माना और संपत्ति की जब्ती तक विविध प्रकार के दंड का प्रावधान किया है। न्यायालयों ने यह सिद्ध किया है कि कठोर दंड केवल “अत्यंत दुर्लभ” मामलों में ही उचित है और बाकी मामलों में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
आधुनिक समय में, अपराध की जड़ों को खत्म करने के लिए शिक्षा, पुनर्वास, और सामाजिक समर्थन जैसे उपाय दंड की प्रक्रिया में शामिल किए जा रहे हैं। यह न केवल अपराधी के जीवन को बदलने में सहायक है, बल्कि समाज की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।