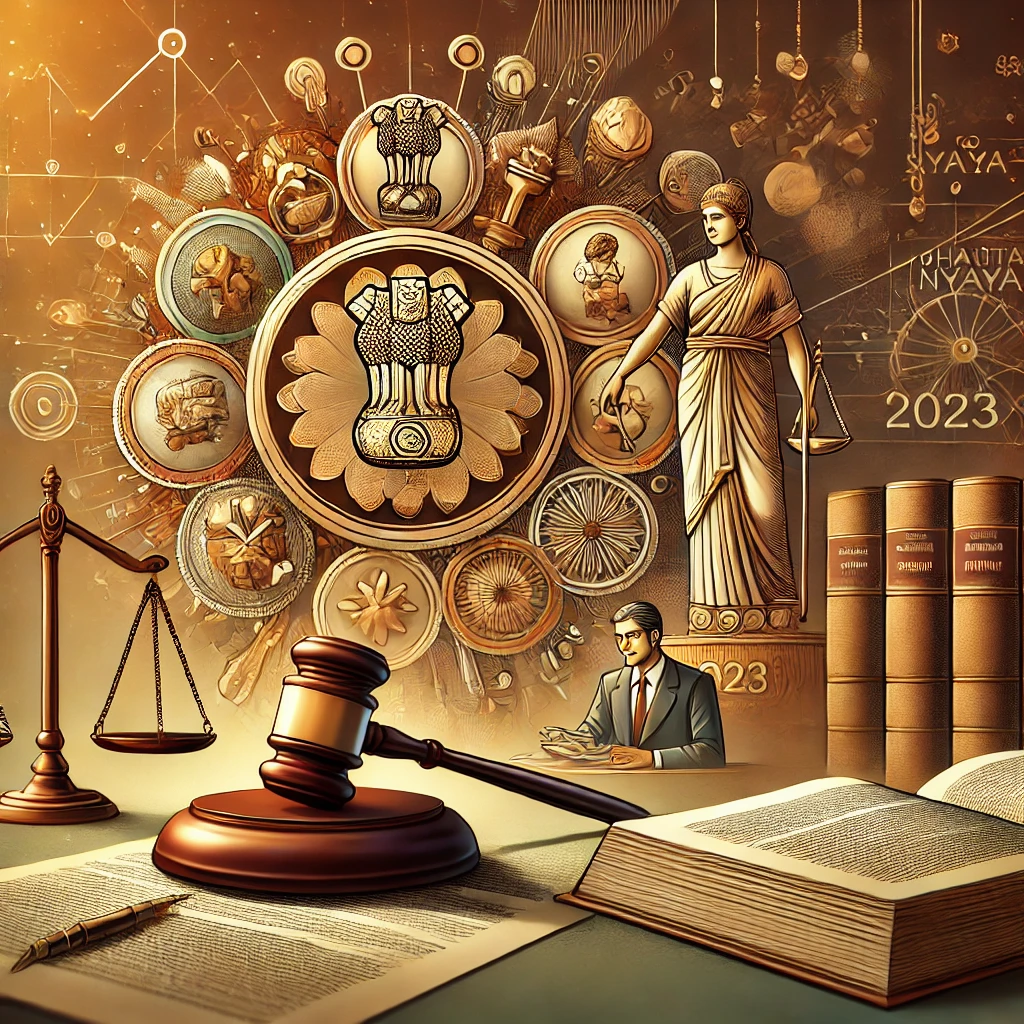लेख शीर्षक: एनपीए और ऋण वसूली कानून: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
(NPA and Debt Recovery Laws in India – Long Article in Hindi)
परिचय
भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक स्थिरता का आधार है, लेकिन समय-समय पर यह विभिन्न वित्तीय संकटों का सामना करती रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख संकट है एनपीए (Non-Performing Assets) की समस्या। एनपीए का बढ़ता बोझ बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता, तरलता और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत में अनेक ऋण वसूली कानून बनाए गए हैं जैसे कि सारफेसी अधिनियम, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम (DRT Act), और हाल ही में लागू इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (IBC), 2016।
इस लेख में हम एनपीए की परिभाषा, इसके प्रकार, कारण, और इससे निपटने के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनी उपायों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
1. एनपीए (Non-Performing Asset) क्या है?
परिभाषा:
एनपीए वह ऋण या अग्रिम होता है, जिसमें निर्धारित तिथि के बाद 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन की कोई वसूली नहीं होती। इसे RBI द्वारा परिभाषित किया गया है।
उदाहरण:
यदि किसी व्यक्ति ने ₹5 लाख का लोन लिया और 3 महीनों तक कोई किश्त या ब्याज नहीं चुकाया, तो यह ऋण NPA घोषित कर दिया जाएगा।
2. एनपीए के प्रकार
- सुब-स्टैंडर्ड एसेट्स (Sub-standard Assets):
ऐसे खाते जो 12 महीनों से कम समय के लिए एनपीए घोषित हुए हैं। - डाउटफुल एसेट्स (Doubtful Assets):
ऐसे खाते जो 12 महीनों से अधिक समय तक एनपीए रहे हैं। - लॉस एसेट्स (Loss Assets):
जिन खातों की वसूली असंभव मानी जाती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह लिखा नहीं गया है।
3. एनपीए के मुख्य कारण
- जानबूझकर ऋण न चुकाना (Wilful Default)
- व्यवसाय में घाटा या दिवालियापन
- प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा या बाढ़
- बैंक की ऋण स्वीकृति में ढिलाई
- आर्थिक मंदी या बाजार में अस्थिरता
4. एनपीए की समस्या के दुष्परिणाम
- बैंक की तरलता (Liquidity) पर असर
- नए ऋण देने की क्षमता में कमी
- ब्याज दरों में वृद्धि
- बैंकिंग क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास कमजोर होना
- आर्थिक विकास की गति में गिरावट
5. ऋण वसूली हेतु प्रमुख कानून
A. ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम, 1993 (RDDBFI Act, अब DRT Act)
उद्देश्य:
बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ₹10 लाख से अधिक की वसूली के मामलों का शीघ्र समाधान।
प्रावधान:
- DRT (Debt Recovery Tribunal) की स्थापना
- DRAT (Appellate Tribunal) अपील के लिए
- केवल बैंक और वित्तीय संस्थाएं ही आवेदन कर सकती हैं
- न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाने हेतु विशेष प्राधिकरण
B. सारफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002)
पूर्ण नाम:
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
मुख्य विशेषताएं:
- ₹1 लाख से अधिक और NPA घोषित खाते पर लागू
- बैंक बिना अदालत की अनुमति के गिरवी संपत्ति को जब्त कर सकता है
- 60 दिन का नोटिस ग्राहक को देना आवश्यक
- Asset Reconstruction Companies (ARC) को अधिकार
महत्वपूर्ण मामला:
Mardia Chemicals Ltd. v. Union of India – सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को SARFAESI के तहत कार्यवाही का अधिकार दिया लेकिन साथ ही न्यायिक संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया।
C. इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (IBC, 2016)
उद्देश्य:
कॉर्पोरेट ऋणों की त्वरित वसूली और दिवालिया कंपनियों का समाधान।
प्रक्रिया:
- NCLT (National Company Law Tribunal) में आवेदन
- 180 दिन (और अधिकतम 330 दिन) में समाधान
- ऋणदाता समिति (Committee of Creditors – COC) द्वारा प्रस्ताव पारित
- कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान या पुनर्गठन
महत्वपूर्ण बिंदु:
IBC ने NPA वसूली के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और बैंकों को कानूनी बल दिया है।
6. अन्य उपाय और पहलें
- RBI द्वारा Prompt Corrective Action (PCA)
- Asset Quality Review (AQR)
- Bad Bank (NARCL) की स्थापना
- IBC में व्यक्तिगत दिवालिया समाधान का प्रावधान
- क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIBIL) के माध्यम से निगरानी
7. न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायपालिका ने ऋण वसूली कानूनों को संविधान-सम्मत ठहराया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया है कि उधारकर्ता के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।
उदाहरण:
- Transcore v. Union of India – एक साथ DRT और SARFAESI की कार्यवाही संभव।
- Swiss Ribbons v. Union of India – IBC को वैध और संतुलित कानून माना गया।
8. निष्कर्ष
एनपीए की समस्या बैंकिंग प्रणाली की एक गंभीर चुनौती है, जिसने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। भारत सरकार और RBI ने इसे नियंत्रित करने के लिए अनेक मजबूत कानून लागू किए हैं – जैसे DRT, SARFAESI और IBC। इन कानूनों ने बैंकों को अदालत से बाहर ऋण वसूली का अधिकार दिया है, जिससे प्रक्रियाओं में गति आई है।
हालांकि, इन कानूनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक, उधारकर्ता, न्यायिक तंत्र और शासन-प्रणाली कितनी प्रभावी और पारदर्शी रूप से कार्य करती है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिससे बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उधारकर्ता को भी न्याय मिले।