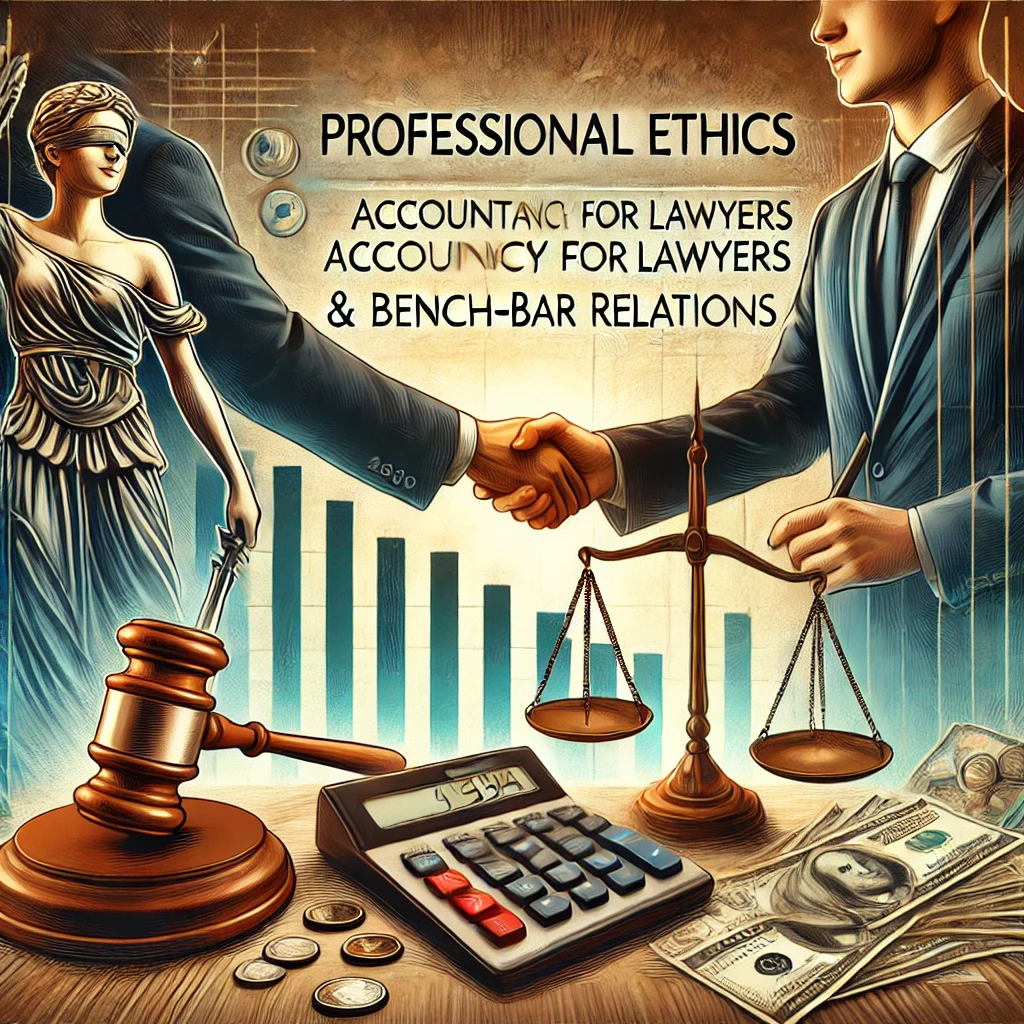न्यायिक आचरण और जवाबदेही (Judicial Ethics and Accountability)
प्रस्तावना (Introduction):
न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसका मुख्य कार्य संविधान और कानूनों के अनुरूप न्याय प्रदान करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। चूँकि न्यायालयों के निर्णय समाज और शासन को गहराई से प्रभावित करते हैं, इसलिए न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक मापदंडों पर खरी उतरे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायिक आचरण (Judicial Ethics) और न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) अत्यंत आवश्यक हैं।
1. न्यायिक आचरण का अर्थ (Meaning of Judicial Ethics):
न्यायिक आचरण से तात्पर्य न्यायाधीशों द्वारा अपने पद का निर्वहन करते समय अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से है। ये आचरण न्यायाधीश की व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों भूमिकाओं में प्रकट होते हैं। न्यायिक आचरण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश निष्पक्ष, ईमानदार, विवेकशील और निर्भीक हों।
न्यायिक आचरण के मूल तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- निष्पक्षता (Impartiality)
- स्वतंत्रता (Independence)
- ईमानदारी (Integrity)
- गोपनीयता (Confidentiality)
- कर्तव्यपरायणता (Diligence)
- न्याय के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment to Justice)
2. न्यायिक जवाबदेही का अर्थ (Meaning of Judicial Accountability):
न्यायिक जवाबदेही का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका और उसमें कार्यरत न्यायाधीश अपने कार्यों, निर्णयों और व्यवहार के लिए जनता, विधायिका और संविधान के प्रति जवाबदेह हों। चूँकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसकी जवाबदेही नैतिकता, आचार संहिता और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
जवाबदेही दो स्तरों पर होती है:
- नैतिक जवाबदेही (Moral Accountability): जो न्यायाधीश की आत्म-निष्ठा और आंतरिक विवेक से संबंधित होती है।
- संवैधानिक जवाबदेही (Constitutional Accountability): जो संसद, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय जैसी संस्थाओं के प्रति होती है।
3. भारत में न्यायिक आचरण के दिशा-निर्देश (Judicial Conduct Guidelines in India):
भारत में न्यायिक आचरण के लिए कोई विशेष विधिक अधिनियम नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख दस्तावेजों और निर्णयों ने दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं:
a) रेस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ (1997):
- सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया गया एक नैतिक दस्तावेज।
- इसमें 16 नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं जिनमें पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, राजनीतिक गतिविधियों से दूरी, हितों के टकराव से बचाव आदि शामिल हैं।
b) बेंच और बार के संबंध (Code of Conduct for Judges):
- न्यायाधीशों को वकीलों से निजी संबंध बनाने या पक्षपातपूर्ण व्यवहार से दूर रहने की सलाह दी गई है।
c) संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217:
- इनमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने (Impeachment) की प्रक्रिया दी गई है, जो उनके जवाबदेह होने का संवैधानिक आधार है।
d) भारत के मुख्य न्यायाधीशों के वक्तव्य:
- कई मुख्य न्यायाधीशों ने समय-समय पर न्यायिक नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता जताई है।
4. न्यायिक जवाबदेही के तंत्र (Mechanisms for Judicial Accountability):
a) महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment):
- संविधान के अनुसार, यदि किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार, गलत आचरण या अक्षमता का आरोप सिद्ध होता है, तो संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और दुर्लभ है; अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है।
b) इन-हाउस प्रोसीजर (In-House Mechanism):
- सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक आंतरिक व्यवस्था विकसित की है, जिसमें यदि किसी न्यायाधीश पर शिकायत हो तो एक आंतरिक समिति उसकी जांच करती है।
c) न्यायिक जवाबदेही विधेयक (Judicial Standards and Accountability Bill):
- 2010 में संसद में पेश यह विधेयक न्यायाधीशों के लिए आचरण के मानक निर्धारित करता है और शिकायतों की जांच के लिए तंत्र प्रस्तावित करता है, किंतु यह अभी तक कानून नहीं बन पाया।
5. न्यायिक नैतिकता के उल्लंघन के प्रभाव (Effects of Violation of Judicial Ethics):
- जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठता है।
- निर्णयों की वैधता पर संदेह उत्पन्न होता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
इसलिए न्यायिक नैतिकता और जवाबदेही को बनाए रखना न्यायपालिका की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है।
6. भारत में प्रमुख उदाहरण (Important Cases and Instances):
- जस्टिस वी. रमास्वामी केस (1993): सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग लाया गया लेकिन वह पारित नहीं हो पाया।
- जस्टिस सौमित्र सेन (कलकत्ता हाईकोर्ट): महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ था, परंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- प्रशांत भूषण बनाम भारत संघ केस (2020): इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की आलोचना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायिक गरिमा की रक्षा पर बल दिया।
7. समाधान और सुधार के सुझाव (Suggestions for Reform):
- न्यायिक जवाबदेही कानून को शीघ्र पारित किया जाए।
- न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाएं सार्वजनिक की जाएं।
- नैतिक शिक्षा एवं आचार संहिता का प्रशिक्षण दिया जाए।
- सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र निकाय बने।
- न्यायालयों में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार (RTI) बढ़ाया जाए।
उपसंहार (Conclusion):
न्यायिक आचरण और जवाबदेही किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ हैं। एक न्यायाधीश का व्यवहार केवल कानून का ही नहीं बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब न्यायपालिका निष्पक्ष, नैतिक और उत्तरदायी होती है, तभी समाज में न्याय के प्रति विश्वास मजबूत होता है।
निष्कर्षतः, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की अंतिम संरक्षक मानी जाती है, वहां न्यायाधीशों का उच्चतम नैतिक स्तर पर रहना और जवाबदेह होना अनिवार्य है। समय की मांग है कि न्यायिक आचरण की स्पष्ट संहिता और उत्तरदायित्व के प्रभावी तंत्र को विधिक रूप से सुदृढ़ किया जाए ताकि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे।