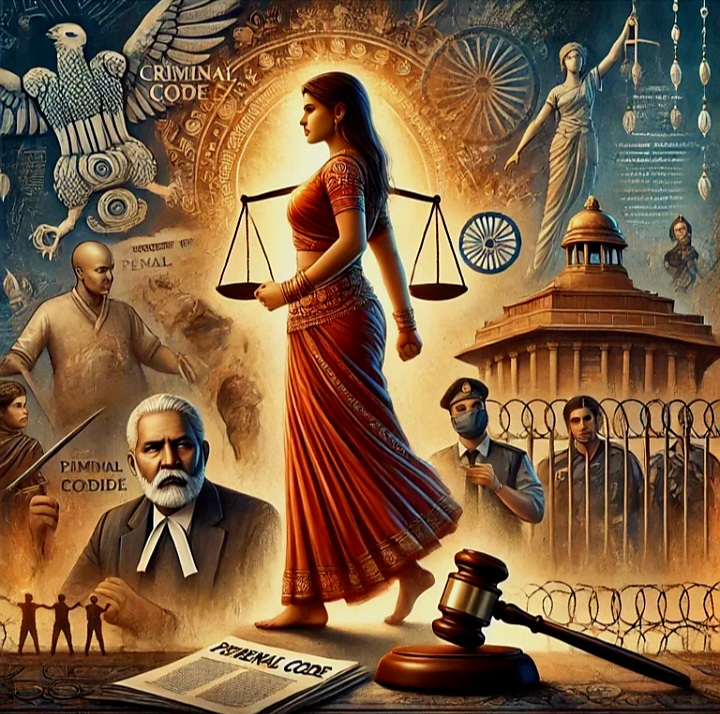✅ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में ‘घरेलू संबंध’, ‘संरक्षण आदेश’ और ‘निवास अधिकार’ की अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए।
परिचय (Introduction):
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का उद्देश्य महिलाओं को उनके परिवार या घरेलू संबंधों में होने वाली हर प्रकार की हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख अवधारणाएँ – घरेलू संबंध, संरक्षण आदेश और निवास का अधिकार – महिलाओं को न केवल सुरक्षा देती हैं बल्कि उनके बुनियादी अधिकारों को भी सुनिश्चित करती हैं।
🟩 1. घरेलू संबंध की अवधारणा (Domestic Relationship):
🔹 धारा 2(f) के अनुसार:
“घरेलू संबंध” से अभिप्राय है, ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें दो व्यक्ति किसी एक ही घरेलू इकाई में रहते हों और:
- वे आपस में विवाह के द्वारा,
- रक्त संबंध से,
- गोद लेने से,
- या लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) द्वारा जुड़े हों।
महत्व:
- यह परिभाषा विवाह तक सीमित नहीं है।
- इसमें ननद, भाभी, सास, दादी, लिव-इन पार्टनर आदि को भी संरक्षण मिल सकता है।
- यह न्यायपालिका को इस अधिनियम के दायरे को व्यापक रूप में लागू करने की शक्ति देता है।
न्यायिक दृष्टांत:
- D. Velusamy v. D. Patchaiammal (2010) – सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव-इन रिलेशनशिप तभी “घरेलू संबंध” मानी जाएगी जब वह विवाह के समकक्ष हो।
🟩 2. संरक्षण आदेश (Protection Orders):
🔹 धारा 18 के अनुसार:
मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि अभियुक्त:
- पीड़िता से किसी प्रकार का संपर्क न करे।
- उसके खिलाफ दोबारा हिंसा न करे।
- उसकी संपत्ति को क्षति न पहुँचाए।
- किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी हिंसा न करे।
महत्व:
- यह आदेश पीड़िता को तुरंत सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह आदेश पुलिस और संरक्षण अधिकारी द्वारा लागू किया जाता है।
- इसका उल्लंघन करने पर आरोपी को एक वर्ष तक की सजा और/या 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है (धारा 31)।
न्यायिक दृष्टांत:
- V.D. Bhanot v. Savita Bhanot (2012) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम उन मामलों पर भी लागू होता है जिनकी घटना इस अधिनियम के लागू होने से पहले की हो।
🟩 3. निवास का अधिकार (Right to Residence):
🔹 धारा 17 और 19 में वर्णित है:
- किसी महिला को वैवाहिक या साझा गृह में रहने का अधिकार है, भले ही वह घर उसके पति या ससुराल वालों के नाम हो।
- मजिस्ट्रेट आरोपी को घर खाली करने, महिला को अलग सुरक्षित आवास देने, या महिला को न निकालने का आदेश दे सकता है।
महत्व:
- महिला को बेघर करने से रोकता है।
- घरेलू हिंसा की स्थिति में उसे मानसिक शांति और आश्रय देता है।
- यह अधिकार कानूनी स्वामित्व पर आधारित नहीं बल्कि संबंध और सहवास पर आधारित होता है।
न्यायिक दृष्टांत:
- S.R. Batra v. Taruna Batra (2007): दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को केवल पति के घर में ही निवास का अधिकार है, न कि सास के स्वामित्व वाले घर में।
निष्कर्ष (Conclusion):
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जरूरी न्यायिक और सामाजिक संरक्षण भी देता है। घरेलू संबंध, संरक्षण आदेश, और निवास अधिकार जैसे प्रावधान इस कानून को महिलाओं के लिए एक सशक्त औजार बनाते हैं। समय-समय पर न्यायपालिका द्वारा दी गई व्याख्याएँ इन प्रावधानों की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को और मजबूत करती हैं।