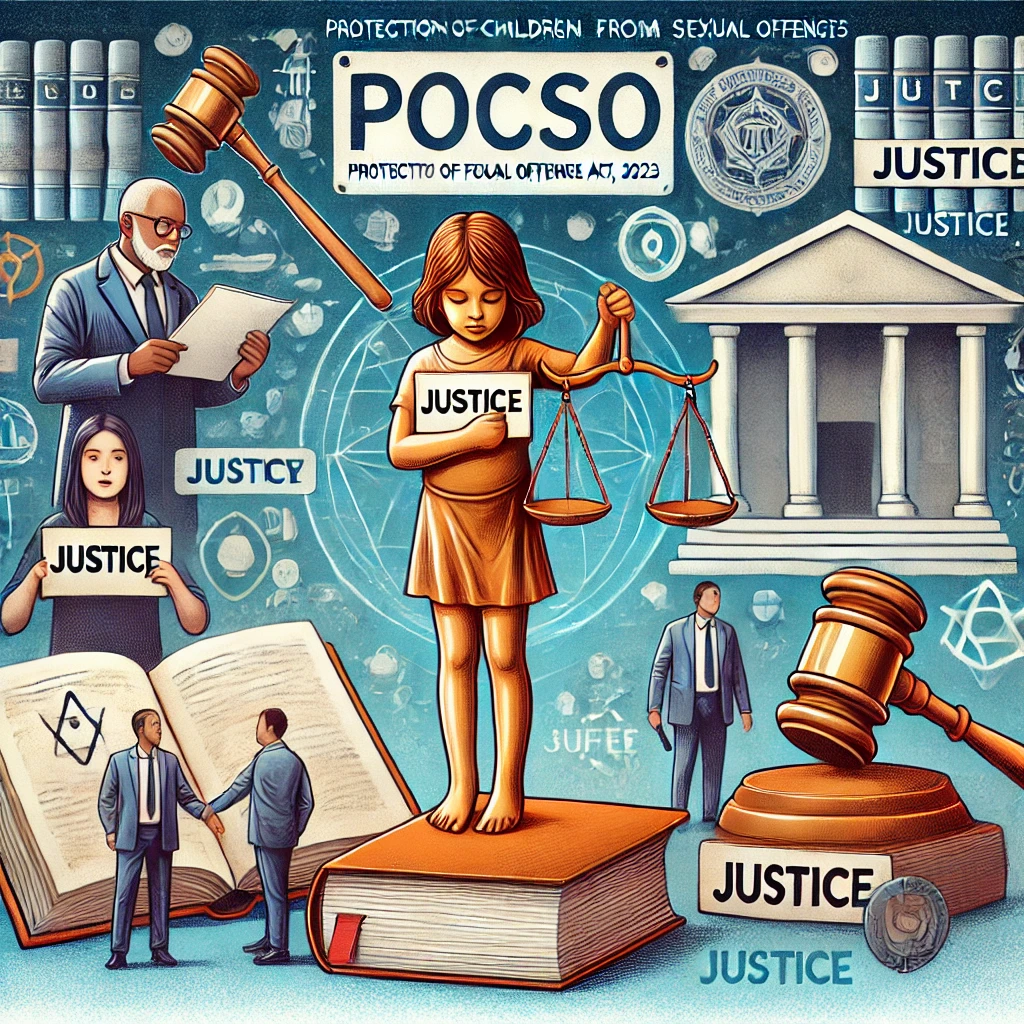“पॉक्सो अधिनियम, 2012 एक विशेष विधि है जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी विशेषताओं, प्रावधानों एवं महत्त्व का वर्णन कीजिए।”
🔶 भूमिका (Introduction):
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में बच्चों की सुरक्षा एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध एक गहरी सामाजिक समस्या है, जो लंबे समय तक छिपी रहती है और न्यायिक संरक्षण से वंचित रह जाती है। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु संसद ने वर्ष 2012 में ‘पॉक्सो अधिनियम’ (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) पारित किया। यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षित करने हेतु एक व्यापक, लैंगिक तटस्थ, और संवेदनशील कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
🔶 अधिनियम का उद्देश्य (Objectives of the Act):
- बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और अश्लीलता से संरक्षण प्रदान करना।
- यौन अपराधों को स्पष्ट परिभाषित करना और उन्हें दंडनीय बनाना।
- न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील, गोपनीय एवं बालहितैषी बनाना।
- विशेष न्यायालयों की स्थापना द्वारा त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।
🔶 प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of the Act):
✅ 1. लैंगिक तटस्थता (Gender Neutrality):
- यह अधिनियम लड़के, लड़की और ट्रांसजेंडर सभी बच्चों पर लागू होता है, जो इसे समावेशी बनाता है।
✅ 2. आयु की सीमा:
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को ‘बच्चा’ मानता है।
✅ 3. अपराधों का वर्गीकरण:
POCSO अधिनियम में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है:
| अपराध | संबंधित धारा | विवरण |
|---|---|---|
| Penetrative Sexual Assault | धारा 3 से 6 | बलात्कार जैसे गंभीर अपराध |
| Sexual Assault | धारा 7 से 9 | शारीरिक संपर्क द्वारा यौन उत्पीड़न |
| Sexual Harassment | धारा 11 से 12 | इशारे, शब्द, अश्लील हरकतें आदि |
| Use of Child for Pornography | धारा 13 से 15 | बाल अश्लीलता का निर्माण या प्रचार |
✅ 4. विशेष न्यायालयों की स्थापना:
- प्रत्येक जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थापना की जाती है जो केवल बच्चों के यौन अपराधों की सुनवाई करती है।
✅ 5. गोपनीय और संवेदनशील प्रक्रिया:
- बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
- बयान महिला अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।
- माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है।
- अदालतें बच्चों से सहजता और गरिमा के साथ प्रश्न करती हैं।
✅ 6. दंड और सजा:
- अपराध की प्रकृति के अनुसार 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है (2019 के संशोधन में)।
- बाल अश्लीलता (child pornography) के लिए कठोर दंड निर्धारित हैं।
🔶 2019 संशोधन (Amendment of 2019):
पॉक्सो अधिनियम को 2019 में और अधिक कठोर और प्रभावी बनाया गया, जिसके तहत:
- बाल बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
- तेजाब हमले, गुदा प्रवेश, और अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को भी शामिल किया गया।
- बाल पोर्नोग्राफी को अपराध मानते हुए कठोर सज़ा तय की गई।
🔶 न्यायालयों की भूमिका और महत्त्वपूर्ण निर्णय:
🔹 State of Maharashtra v. Bandu (2013):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालक की स्पष्ट और विश्वसनीय गवाही, सजा के लिए पर्याप्त है।
🔹 Alakh Alok Srivastava v. Union of India (2018):
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और सक्षम काउंसलिंग तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया।
🔶 अधिनियम की महत्ता (Importance of the Act):
- बाल यौन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा और सख्त सजा।
- बच्चों की गरिमा और मनोवैज्ञानिक स्थिति का संरक्षण।
- न्यायिक प्रणाली में बच्चों के अनुकूल वातावरण।
- लैंगिक समानता और समावेशी दृष्टिकोण।
🔶 चुनौतियाँ और आलोचनाएं:
| चुनौती | विवरण |
|---|---|
| कम रिपोर्टिंग | सामाजिक बदनामी और डर के कारण कई मामले दर्ज नहीं होते। |
| झूठे मामले | कुछ मामलों में कानून का दुरुपयोग होता है। |
| प्रशिक्षण की कमी | पुलिस और न्यायाधीशों को बच्चों से संबंधित मामलों की संवेदनशीलता का ज्ञान कम होता है। |
| मुकदमों में देरी | विशेष अदालतों की कमी के कारण निर्णय में विलंब होता है। |
🔶 सुझाव (Suggestions):
- जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि लोग इस कानून के प्रावधानों को समझ सकें।
- पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
- स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य किया जाए।
- बच्चों के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।
🔶 निष्कर्ष (Conclusion):
पॉक्सो अधिनियम, 2012 भारत सरकार की एक सशक्त विधिक पहल है, जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए समर्पित है। यह अधिनियम न केवल दंडात्मक है, बल्कि रक्षात्मक, संवेदनशील और पुनर्वास-उन्मुख भी है। इसकी प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित होगी जब कानून का सख्त पालन, समाज की जागरूकता, और संवेदनशील प्रशासनिक मशीनरी एक साथ कार्य करें। बच्चों की सुरक्षा केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।