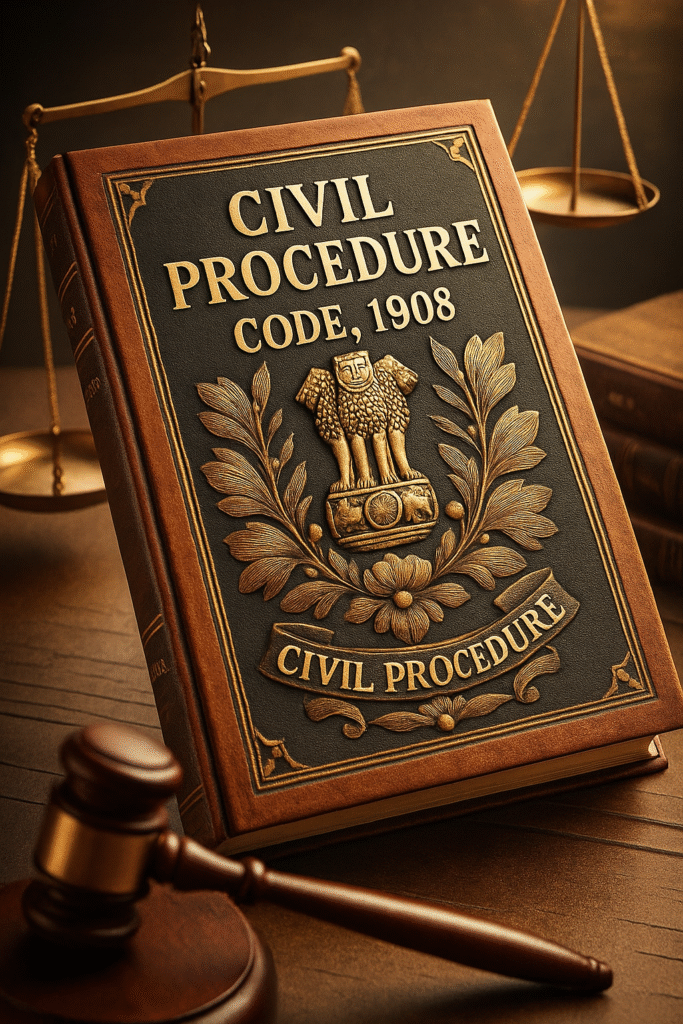नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 क्या है? इसकी संरचना, उद्देश्य तथा प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए।
परिचय (Introduction):
न्याय एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व और न्यायप्रियता प्रदान करता है। भारत में दीवानी (सिविल) मामलों में न्याय दिलाने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका निर्धारण “नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908” द्वारा किया जाता है। यह संहिता दीवानी मामलों की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक एवं संगठित विधिक दस्तावेज है।
संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
ब्रिटिश शासन काल में दीवानी न्याय की प्रक्रिया क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न थी, जिससे असमानता उत्पन्न होती थी। इसलिए न्यायिक प्रणाली में एकरूपता लाने हेतु 1908 में नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) अधिनियमित की गई। यह संहिता 1 जनवरी 1909 से प्रभाव में आई। यह पहले की संहिताओं जैसे – 1859, 1877 और 1882 की संहिताओं का स्थान लेती है।
नागरिक प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य:
- न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता लाना।
- सभी पक्षों को न्याय दिलाने हेतु समान अवसर प्रदान करना।
- वादों की निष्पक्ष, त्वरित एवं कुशल सुनवाई को सुनिश्चित करना।
- अपील, पुनरीक्षण, निष्पादन आदि विधियों द्वारा पूर्ण न्याय प्रदान करना।
- न्यायालय की शक्तियों, क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया व अधिकारों का विनियमन करना।
संरचना (Structure of CPC):
CPC दो मुख्य भागों में विभाजित है:
(क) धाराएं (Sections):
- कुल 158 धाराएं (Sections 1 to 158) हैं।
- ये न्यायालयों की शक्तियों, अधिकार क्षेत्र, वादों के प्रारंभ, अपील, पुनरीक्षण, निषेधाज्ञा आदि से संबंधित हैं।
(ख) आदेश एवं नियम (Orders and Rules):
- कुल 51 आदेश (Orders I to LI) हैं।
- प्रत्येक आदेश के अधीन संबंधित नियम होते हैं, जिनमें दीवानी मुकदमों की संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जैसे वाद पत्र, समन, साक्ष्य, निष्पादन आदि।
प्रमुख धाराएं और आदेश:
| क्रमांक | धारा/आदेश | विषयवस्तु |
|---|---|---|
| 1 | धारा 9 | दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र |
| 2 | धारा 10 | Res Sub Judice – वाद लंबित होने पर पुनः वाद निषिद्ध |
| 3 | धारा 11 | Res Judicata – पूर्व निर्णय बाध्यकारी होता है |
| 4 | धारा 80 | सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध वाद से पूर्व सूचना |
| 5 | आदेश 1 | आवश्यक पक्षकार |
| 6 | आदेश 7 | वाद पत्र की सामग्री |
| 7 | आदेश 9 | अनुपस्थिति में निर्णय |
| 8 | आदेश 20 | निर्णय और डिक्री |
| 9 | आदेश 21 | डिक्री का निष्पादन |
| 10 | आदेश 39 | अस्थायी निषेधाज्ञा |
नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रमुख सिद्धांत (Key Principles):
- Natural Justice (प्राकृतिक न्याय)
सभी पक्षों को सुनवाई का समान अवसर दिया जाता है। - Res Judicata (पूर्वविवाद निवारण)
एक बार जिस विवाद का निर्णय हो चुका है, उसे पुनः नहीं खोला जा सकता। - Sub Judice (वाद लंबितता सिद्धांत)
एक ही विवाद समान पक्षों के बीच यदि पहले से लंबित है, तो पुनः मुकदमा नहीं किया जा सकता। - Audi Alteram Partem
“दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं” – निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत। - Judicial Discipline and Hierarchy
अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों से बाध्य रहते हैं।
महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं (Judicial Interpretations):
- Satyadhyan Ghosal v. Deorajin Debi (AIR 1960 SC 941):
Res Judicata की सीमा और प्रयोजन स्पष्ट किया गया। - Salem Advocate Bar Association v. Union of India (2005):
2002 के संशोधनों की वैधता तथा ADR (वैकल्पिक विवाद समाधान) की महत्ता पर बल।
संशोधन और नवीन पहल:
- 2002 संशोधन:
प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने हेतु अनेक बदलाव किए गए – जैसे, समयबद्ध सुनवाई, गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग आदि। - डिजिटल युग में CPC:
ई-फाइलिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग, ई-समन जैसे प्रावधानों से CPC को तकनीकी रूप में उन्नत किया जा रहा है।
निष्कर्ष (Conclusion):
नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 केवल एक तकनीकी कानून नहीं है, बल्कि यह न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाला मौलिक विधिक उपकरण है। यह न्यायालयों की कार्यवाही को एक नियमानुसार ढांचे में संचालित करता है ताकि नागरिकों को शीघ्र, सुलभ और न्यायसंगत राहत मिल सके। समयानुसार इसके संशोधन और व्याख्याएं इसे और भी प्रासंगिक बनाते हैं। यह निःसंदेह भारतीय विधिक प्रणाली की रीढ़ है।