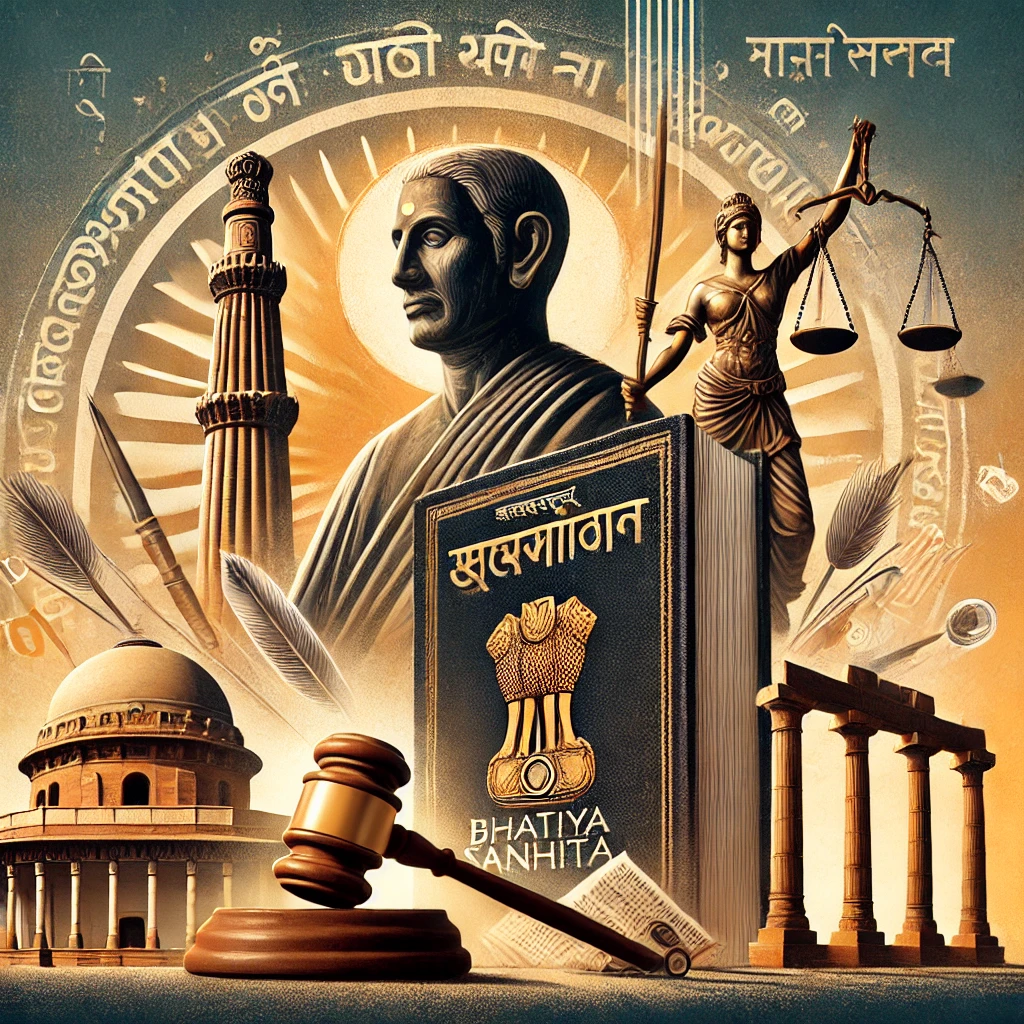शीर्षक: आभासी अदालतें (Virtual Courts): स्थायी समाधान या अस्थायी व्यवस्था? – भारतीय न्याय प्रणाली की डिजिटल दिशा में एक विवेचनात्मक विश्लेषण
🔷 प्रस्तावना:
भारत की न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ करोड़ों मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। ऐसे में तकनीक की सहायता से न्यायिक कार्यवाही को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाने के प्रयास समय की माँग हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान एक असाधारण प्रयोग हुआ – न्यायालयों को वर्चुअल (आभासी) माध्यम से संचालित करना पड़ा। यह प्रयोग आपातकालीन परिस्थिति में शुरू हुआ, लेकिन अब इसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि – क्या आभासी अदालतें न्याय प्रणाली का स्थायी समाधान बन सकती हैं या यह केवल अस्थायी विकल्प है?
🔷 आभासी अदालतें क्या हैं?
आभासी अदालतें वे मंच हैं जहाँ मुकदमों की सुनवाई भौतिक रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-फाइलिंग, ऑनलाइन प्रस्तुतियाँ और डिजिटल आदेशों के माध्यम से होती है। इसमें न्यायाधीश, वकील, वादी और प्रतिवादी अपने-अपने स्थानों से जुड़े रहते हैं।
भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों और कई जिला न्यायालयों ने “e-Courts परियोजना” के तहत डिजिटल माध्यम अपनाया है।
🔷 आभासी अदालतों की उपलब्धियाँ:
- न्याय की सुलभता:
दूरदराज़ के क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक यात्रा किए बिना न्याय मिलना आसान हुआ। - समय और संसाधनों की बचत:
यात्रा, प्रतीक्षा और दस्तावेज़ों की छपाई से संबंधित खर्चों में कटौती हुई। - महामारी के समय न्यायिक निरंतरता:
लॉकडाउन के दौरान भी अदालतें बंद नहीं हुईं — यह भारतीय न्याय प्रणाली की लचीलापन (resilience) का प्रमाण बना। - ई-फाइलिंग और पेपरलेस कोर्ट:
दस्तावेजों का डिजिटल प्रस्तुतीकरण और आर्काइविंग सरल हुआ, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। - कारगर त्वरित सुनवाई:
जमानत याचिकाओं, अंतरिम आदेशों, और अल्पकालिक मामलों में तेजी से निर्णय हुए।
🔷 स्थायी समाधान के रूप में आभासी अदालतें – संभावनाएँ:
- डिजिटल इंडिया मिशन को बल:
न्यायपालिका की डिजिटल पहल प्रधानमंत्री के “डिजिटल इंडिया” दृष्टिकोण के अनुरूप है। - ई-गवर्नेंस का विस्तार:
न्यायिक क्षेत्र में तकनीक के विस्तार से ई-गवर्नेंस की पहुँच व्यापक हो सकती है। - न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता:
रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग और ई-ऑर्डर्स से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी। - विकसित देशों की तर्ज पर न्याय प्रणाली:
अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पहले से ही डिजिटल कोर्ट्स की स्थायी व्यवस्था विकसित हो चुकी है। भारत भी उसी दिशा में अग्रसर हो सकता है।
🔷 आभासी अदालतों की सीमाएँ और चुनौतियाँ:
- डिजिटल विभाजन (Digital Divide):
ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण समान न्याय तक पहुँच सीमित हो जाती है। - प्रभावी मौखिक बहस की बाधा:
स्क्रीन के माध्यम से न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच भावनात्मक और दलीय प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता जितना आमने-सामने होता है। - तकनीकी समस्याएँ:
नेटवर्क की अस्थिरता, खराब वीडियो/ऑडियो गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे सुनवाई में बाधा डालते हैं। - गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का प्रश्न:
वीडियो सुनवाई, दस्तावेजों की ऑनलाइन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग से डेटा लीक और साइबर अटैक की आशंका बनी रहती है। - न्यायिक अनुभव की गुणवत्ता में गिरावट:
न्यायाधीश को प्रत्यक्ष रूप से गवाहों, वादियों और अधिवक्ताओं के हावभाव, व्यवहार और आचरण का आकलन करने में कठिनाई होती है।
🔷 न्यायपालिका और बार की दृष्टिकोण:
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने वर्चुअल कोर्ट को आधुनिक न्याय प्रणाली का आवश्यक अंग बताया है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि सभी मामलों में इसे लागू करना अभी व्यवहारिक नहीं।
- बार काउंसिल और वरिष्ठ वकीलों की राय है कि वर्चुअल सुनवाई केवल कुछ प्रकार के मामलों के लिए ही उपयुक्त है जैसे – जमानत याचिका, स्टे ऑर्डर, अंतरिम आवेदन, आदि।
- कई वकील विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवक्ताओं ने वर्चुअल व्यवस्था के प्रति असहमति जताई, यह कहते हुए कि यह समान अवसर और पेशेवर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।
🔷 अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:
- यूके: COVID-19 के बाद भी कई मामलों में वर्चुअल हियरिंग जारी है।
- ऑस्ट्रेलिया: डिजिटल कोर्ट प्रक्रिया नियमित न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बन चुकी है।
- चीन: इंटरनेट कोर्ट्स की स्थापना हुई है, जहाँ पूरा ट्रायल डिजिटल रूप में होता है।
भारत को इन मॉडलों से सीखते हुए हाइब्रिड व्यवस्था (Hybrid System) की ओर बढ़ना चाहिए।
🔷 भविष्य की राह: हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता
- सभी मामलों में नहीं, चयनात्मक उपयोग:
वर्चुअल सुनवाई को केवल आवश्यक मामलों में लागू किया जाए – जैसे बेल, अर्जेंसी, डॉक्यूमेंट्री सुनवाई आदि। - तकनीकी ढाँचे का सशक्तिकरण:
हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल कोर्टरूम, साइबर सुरक्षा और प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी सुनिश्चित किए जाएँ। - डिजिटल साक्षरता अभियान:
वकीलों, न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों को तकनीक के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक बनाना आवश्यक है। - डाटा गोपनीयता कानून का निर्माण:
अदालतों में उपयोग हो रही डिजिटल प्रणालियों के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा कानून की तत्काल आवश्यकता है। - समान न्याय के सिद्धांत का पालन:
आभासी व्यवस्था से कोई वर्ग या क्षेत्र न्याय से वंचित न हो — यह सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।
🔷 निष्कर्ष:
आभासी अदालतें कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि भविष्य की न्याय प्रणाली का एक अभिन्न भाग बन चुकी हैं। हालाँकि यह एक सम्पूर्ण विकल्प नहीं है, लेकिन यदि इसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और न्यायिक दृष्टिकोण से समर्पित तकनीकी ढाँचे के साथ लागू किया जाए, तो यह न्यायिक दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता को नई ऊँचाई दे सकता है। भारत को अब एक हाइब्रिड और समावेशी मॉडल की दिशा में सोचना होगा, जहाँ पारंपरिक न्याय प्रणाली और डिजिटल नवाचारों का समन्वय हो।