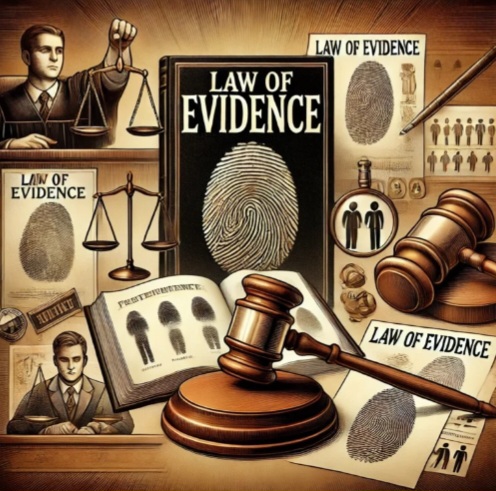शीर्षक: डिजिटल साक्ष्य और उनकी स्वीकार्यता: कानूनी बारीकियाँ और न्यायिक दृष्टिकोण
🔷 प्रस्तावना:
डिजिटल युग में अपराध, अनुबंध, धोखाधड़ी और प्रशासनिक कार्यों का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साक्ष्य (Electronic Evidence) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ई-मेल, सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज, वॉयस रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट्स, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव आदि आधुनिक डिजिटल उपकरणों से प्राप्त साक्ष्य अब न्यायालयों में दलीलों का प्रमुख आधार बनते जा रहे हैं। लेकिन इन साक्ष्यों की स्वीकार्यता (admissibility), प्रमाणिकता (authenticity) और कानूनी वैधता को लेकर कई जटिलताएं और बारीकियाँ जुड़ी हुई हैं।
🔷 डिजिटल साक्ष्य की परिभाषा और प्रकार:
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है और धारा 65B में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता का विस्तृत प्रावधान है। डिजिटल साक्ष्य वे सभी सूचनाएं हैं जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न, संग्रहीत या संचारित होती हैं। इनके प्रमुख प्रकार हैं:
- ई-मेल्स और व्हाट्सएप चैट्स
- ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग
- सीसीटीवी फुटेज
- सोशल मीडिया पोस्ट
- वेबसाइट स्क्रीनशॉट
- हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव आदि
- कॉल रिकॉर्ड्स और GPS डेटा
🔷 भारतीय कानून में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता:
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B:
यह धारा स्पष्ट करती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में स्वीकार्य बनाने के लिए उसे 65B(4) प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो उस कंप्यूटर सिस्टम का प्रभारी हो जिससे साक्ष्य प्राप्त हुआ हो। - धारा 22A:
मौखिक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में हों और रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो। - धारा 45A:
डिजिटल साक्ष्य से संबंधित विशेषज्ञ की राय भी अदालत में महत्वपूर्ण होती है। यदि साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ किसी डिजिटल रिकॉर्ड की प्रमाणिकता की पुष्टि करता है, तो वह मान्य माना जाता है। - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
यह कानून डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षा, प्रमाणीकरण, साइबर अपराध, डेटा हैकिंग आदि से संबंधित है और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ पूरक रूप में कार्य करता है।
🔷 प्रमुख न्यायिक निर्णय:
- State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu (Parliament Attack Case, 2005):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 65B प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो अन्य साक्ष्यों के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि यह निर्णय बाद में संशोधित किया गया। - Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014) 10 SCC 473:
यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए धारा 65B(4) प्रमाणपत्र अनिवार्य है। इसके बिना साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। - Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020):
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष डिजिटल साक्ष्य पेश कर रहा है तो 65B प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है, चाहे मूल स्रोत पक्ष के पास हो या न हो।
🔷 डिजिटल साक्ष्य की प्रमाणिकता और चुनौतियाँ:
- संपादन की संभावना:
डिजिटल रिकॉर्ड को एडिट, डिलीट या मॉर्फ किया जा सकता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। - सोर्स की पहचान:
साक्ष्य किस सिस्टम से प्राप्त हुआ, किसने उसे जनरेट किया – यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है। - टाइम स्टैम्प और मेटाडेटा:
डिजिटल फाइल का वास्तविक समय, IP एड्रेस, मेटाडेटा आदि भी प्रमाणिकता को प्रमाणित करने में सहायक होते हैं। - फॉरेंसिक जांच:
डिजिटल साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले साइबर फॉरेंसिक जांच कराना अक्सर आवश्यक होता है ताकि हेरफेर की संभावना समाप्त हो।
🔷 न्यायालयों में व्यवहारिक समस्याएँ:
- अधिकांश अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी अभी भी डिजिटल साक्ष्य की तकनीकी बारीकियों से भलीभांति परिचित नहीं हैं।
- फॉरेंसिक विशेषज्ञों की संख्या सीमित है और रिपोर्ट में विलंब होता है।
- पुलिस विभाग में तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण डिजिटल साक्ष्य सही ढंग से संरक्षित नहीं हो पाते।
- कई बार आरोपी पक्ष 65B प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति को लेकर तकनीकी आधार पर मुकदमा खारिज कराने का प्रयास करता है।
🔷 सुधार की आवश्यकता:
- न्यायिक प्रशिक्षण:
न्यायिक अधिकारियों को नियमित रूप से डिजिटल साक्ष्य और साइबर कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। - 65B प्रमाणपत्र की प्रक्रिया सरल बनाना:
छोटे मामलों में साक्ष्य देने वाले को अधिक बोझिल प्रक्रियाओं से बचाते हुए प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। - फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण:
सभी राज्यों में अत्याधुनिक साइबर लैब स्थापित की जानी चाहिए ताकि डिजिटल साक्ष्य का परीक्षण शीघ्र हो सके। - डिजिटल सुरक्षा मानकों का निर्धारण:
डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने के लिए डेटा इंटीग्रिटी और ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था होनी चाहिए।
🔷 निष्कर्ष:
डिजिटल साक्ष्य आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ये पारंपरिक साक्ष्यों की तुलना में अधिक विस्तृत, सटीक और तत्काल होते हैं, लेकिन इनकी स्वीकार्यता न्यायालय में तभी संभव है जब वे कानूनी मानकों को पूर्ण करें। धारा 65B और अन्य संबंधित प्रावधानों को सही ढंग से लागू करना, न्यायिक और प्रशासनिक सुधार करना तथा डिजिटल जागरूकता बढ़ाना समय की मांग है। जब तक न्यायिक प्रणाली तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठाएगी, तब तक डिजिटल साक्ष्य की पूर्ण स्वीकार्यता संभव नहीं होगी।