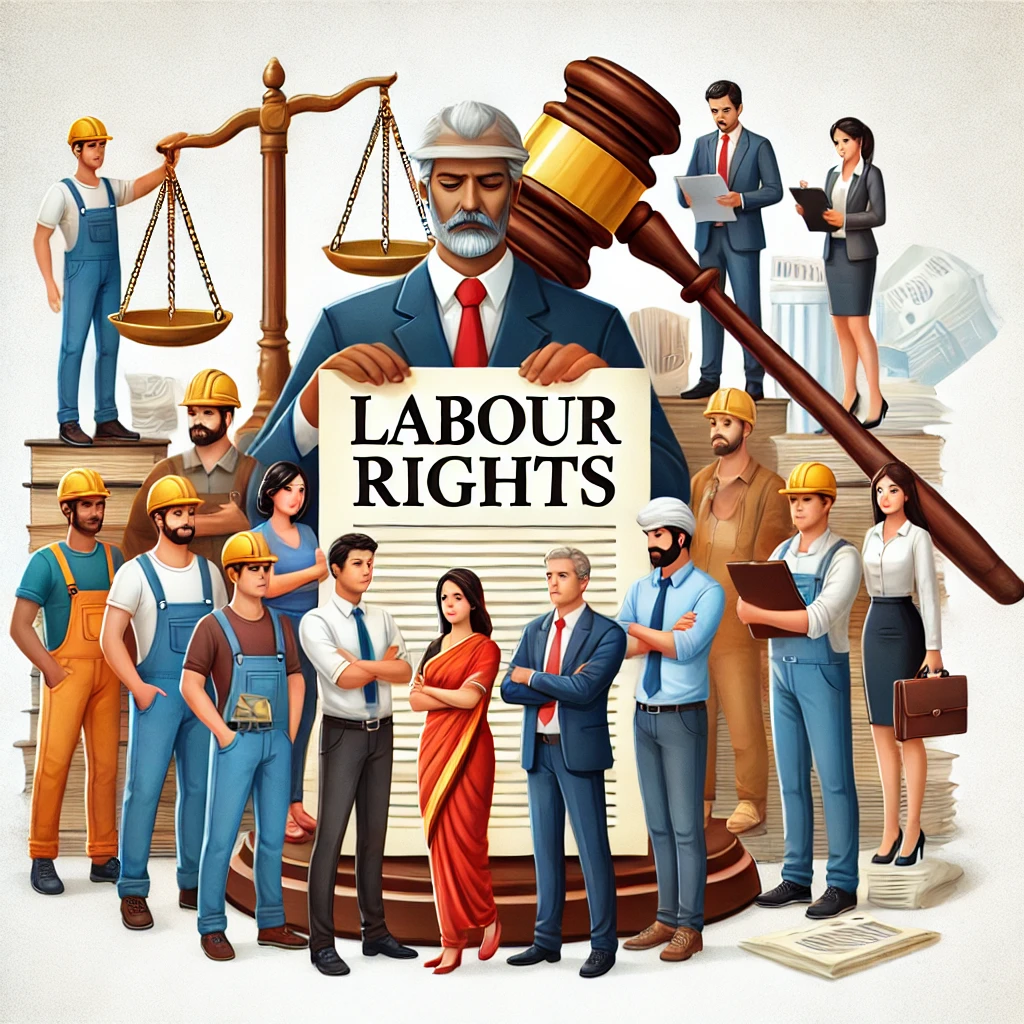शीर्षक: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 : श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा का संवैधानिक आधार
परिचय
भारत जैसे विकासशील देश में जहां श्रमिकों की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है, वहां उनके आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। श्रमिकों को समय पर उचित मजदूरी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए “मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936” (Payment of Wages Act, 1936) को लागू किया गया। यह अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम था, जो श्रमिकों को नियोक्ताओं की मनमानी से बचाने के लिए लाया गया।
अधिनियम का उद्देश्य
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को उनकी अर्जित मजदूरी—
- समय पर
- पूर्ण रूप से
- और कानूनी रूप से मान्य माध्यमों द्वारा
प्राप्त हो। यह अधिनियम न केवल वेतन भुगतान के समय-सीमा को निर्धारित करता है, बल्कि अवैध कटौतियों पर भी रोक लगाता है।
प्रमुख परिभाषाएं
- मजदूरी (Wages): किसी कर्मचारी को उसके काम के लिए दी जाने वाली सैलरी, बोनस, भत्ता, छुट्टियों का वेतन आदि।
- नियोक्ता (Employer): वह व्यक्ति या संस्था जो श्रमिकों को रोजगार देती है।
- कर्मचारी (Employee): वह व्यक्ति जो नियोक्ता के अधीन वेतन के बदले कार्य करता है।
अधिनियम के अंतर्गत लागू क्षेत्र
यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ—
- 1000 या उससे अधिक कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ हो, या
- सरकार द्वारा अधिसूचित कोई विशेष उद्योग हो।
शुरुआत में यह अधिनियम ₹1000 प्रति माह कमाने वाले श्रमिकों तक सीमित था, परंतु समय-समय पर इसमें संशोधन कर सीमा को बढ़ाया गया है।
वेतन भुगतान की समय-सीमा
अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान—
- 10 या उससे कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है।
- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन देना आवश्यक है।
वैध कटौतियाँ (Authorized Deductions)
नियोक्ता कुछ विशेष परिस्थितियों में वेतन से कटौती कर सकता है, जैसे:
- आयकर
- कर्मचारी राज्य बीमा (ESI)
- भविष्य निधि (PF)
- अनुपस्थिति के कारण कटौती
- दंडात्मक कार्रवाई (जैसे अनुशासनहीनता)
महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कटौतियाँ अधिनियम के दायरे में वैध होनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
अवैध कटौतियों पर प्रतिबंध
अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियोक्ता किसी भी प्रकार की मनमानी कटौती नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारी लेबर इंस्पेक्टर या मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिकायत और न्याय प्रणाली
यदि किसी कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता या अवैध कटौती की जाती है, तो वह निम्नलिखित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है:
- प्राधिकृत अधिकारी (Authority appointed under the Act)
- लेबर इंस्पेक्टर
- मजिस्ट्रेट (अक्सर प्रथम श्रेणी)
शिकायत करने की समय-सीमा वेतन के भुगतान की नियत तिथि से 12 माह के भीतर है।
दंडात्मक प्रावधान
यदि नियोक्ता अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे निम्न दंड दिए जा सकते हैं:
- पहली बार उल्लंघन पर ₹20,000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की सजा।
- बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक कठोर दंड।
यह प्रावधान श्रमिकों को नियोक्ता के शोषण से बचाने के लिए आवश्यक हैं।
संशोधन एवं अद्यतन
मजदूरी भुगतान अधिनियम में समय-समय पर कई संशोधन किए गए हैं ताकि इसका दायरा और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। कोड ऑन वेजेज, 2019 (Code on Wages, 2019) के अंतर्गत इस अधिनियम को चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) में सम्मिलित कर दिया गया है, जो मजदूरों के लिए एकीकृत और सरल कानून बनाने की दिशा में कदम है।
अधिनियम का सामाजिक महत्व
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 भारत में श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला पहला मजबूत कानून था। इस अधिनियम ने यह सिद्ध कर दिया कि—
- श्रमिक केवल श्रम का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं।
- उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार और समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 भारतीय श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रभावी कदम रहा है। इसने समय पर वेतन की गारंटी देकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राहत दी है। हालाँकि नए श्रम संहिता कानूनों के अंतर्गत इसे विलीन कर दिया गया है, फिर भी इसकी मूल भावना आज भी श्रमिक न्याय के स्तंभ के रूप में जीवित है।