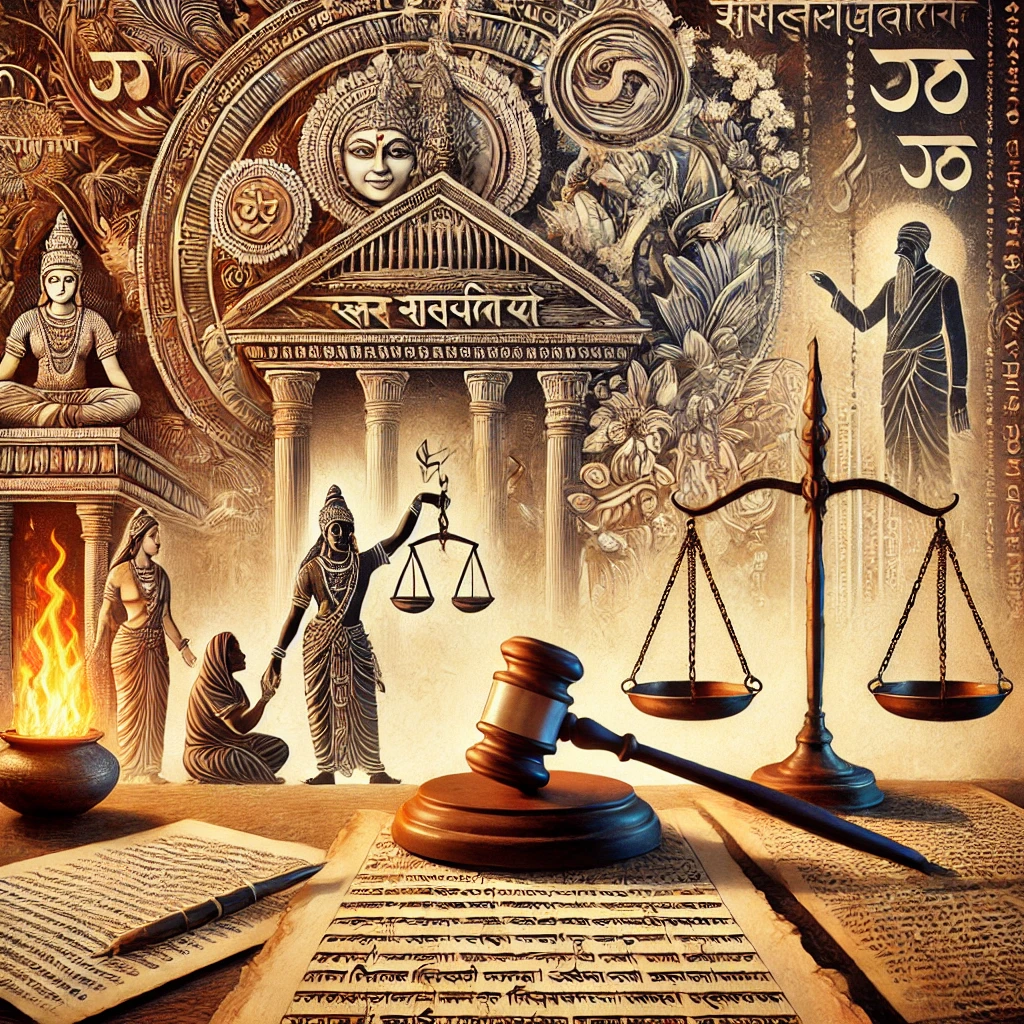प्रश्न 20. संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता के अन्य संक्रामण की शक्तियों की समीक्षा कीजिए।
Critically examine the powers of alienation by Karta of Joint Hindu Family.
उत्तर – कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण किया जा सकता है। अन्य सक्रांमण में विक्रय, दान, बन्धक, पट्टा तथा आदान प्रदान भी सम्मिलित है। अन्य संक्रामण कर्त्ता द्वारा अथवा प्रबन्धक द्वारा विधिक आवश्यकता अथवा सम्पदा के प्रलाभ के लिए किया जा सकता है। जब अन्य सहदायिक परिवार में वयस्क होते हैं तो उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही अन्य संक्रामण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पिता को (कर्त्ता को) कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये जाते हैं
कर्त्ता द्वारा विधिक आवश्यकता अथवा सम्पदा के प्रलाभ के लिए अन्य संक्रामण- जब परिवार के सदस्य अवयस्क होते हैं तो कर्त्ता संयुक्त अविभक्त सम्पत्ति को •आपत्तियों से बचाव में तथा परिवार की भलाई एवं कल्याण के लिए अन्यसंक्रामित कर सकता है जिससे वह स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्य बाधित होते हैं अत: संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का अन्य संक्रामण विधिक आवश्यकता अथवा सम्पदा के प्रलाभ के लिए ही हो सकता है।
विधिक आवश्यकता– विधिक आवश्यकता का प्रयोग उस अर्थ में किया जाता है। जहाँ संयुक्त परिवार को कोई प्राधिकृत सदस्य किसी परिस्थिति में सम्पत्ति के स्वामित्व को दूसरे के हाथ में देता है। निम्नलिखित बातें विधिक आवश्यकता की कोटि में रखी जाती है।
(1) राजस्व तथा ऋणों को चुकाना जो परिवार के ऊपर है।
(2) सहदायिकों तथा उनके परिवार का भरण-पोषण।
(3) सहदायिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह का खर्च।
(4) श्राद्ध कर्म, मृतक संस्कार तथा धार्मिक अनुष्ठानों के खर्च।
(5) परिवार के आवश्यक मुकदमों के खर्च।
(6) परिवार के लिए निवासगृह बनवाने का व्यय तथा निवासगृह की मरम्मत के व्यय।
(7) परिवार में अंशों के उचित वितरण के लिए परिवार की किसी सम्पत्ति का व्यय करना ।
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वनीमिसाती अनिल कुमार बनाम जयवरापू कृष्णमूर्ति, ए० आई० आर० (1995) आन्ध्र प्रदेश 105 के बाद में कहा कि कर्त्ता द्वारा परिवार के सदस्यों को बेहतर जीवन यापन करने के लिए अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में सम्पत्ति को बेचना अथवा पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी के लिए सम्पत्ति बेचना विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत आयेगा।
(1) सम्पदा के प्रलाभ- सम्पदा के प्रलाभ के लिए भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का अन्य-संक्रामण किया जा सकता है। प्रिवी कौंसिल ने निम्न को सम्पदा के लाभ के सम्बन्ध में कहा है-सम्पत्ति की लुप्त होने से प्रतिरक्षा करना, गम्भीर बाद में प्रतिरक्षा करना, क्षति अथवा ‘ निर्मूलन से पूरी सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश की रक्षा करना तथा इसी प्रकार की बातें जो सम्पदा के प्रलाभ से सम्बन्ध रखती हैं। व्यापक अर्थ में विधिक आवश्यकता सम्पदा के प्रलाभ को भी सम्मिलित करती है।
हरि सिंह बनाम उमराव सिंह, ए० आई० आर० (1979) इलाहाबाद 65 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ संयुक्त परिवार की ऐसी सम्पत्ति को, जिससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था, बेचकर सस्ते भाव में कहीं भूमि खरीदी गई जिससे अधिक लाभ हो सकता है वहाँ ऐसे अन्य संक्रामण को वैध ठहराया जायेगा। अन्य संक्रामण उसके परिवार के लाभ के लिए दूसरे शब्दों सम्पदा के प्रलाभ के लिए समझा जायेगा।
(2) सभी सहदायिकों की सहमति से अन्य संक्रामण– यदि परिवार के अन्य सदस्य वयस्क हैं तथा अन्यसंक्रामण बिना किसी विधिक आवश्यकता अथवा सम्पदा के प्रलाभ की दृष्टि से किया गया है, किन्तु वयस्क सदस्यों की पूर्वस्वीकृति ली जा चुकी है तो उस दशा में भी अन्यसंक्रामण मान्य होगा। प्रिवी कौंसिल ने उल्लेख किया है कि “कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अन्य सदस्यों को स्वीकृति नहीं प्राप्त कर ली जाती” यदि वे सदस्य इस प्रकार की स्वीकृति दे सकते थे। स्वीकृति स्पष्ट अथवा अस्पष्ट हो सकती है। अतः परिवार के कर्त्ता द्वारा अन्य सहदायिकों की स्वीकृति के बिना अन्यसंक्रामण दान अथवा इच्छापत्र से करना पूर्णतया शून्य होगा न कि शून्यकरणीय संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा बिना किसी विधिक आवश्यकता के सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण बन्धक से अथवा विक्रय करके शुन्यकरणीय होगा जो दूसरे सहदायिकी की इच्छा पर निर्भर करेगा। यू० जी० श्रीनिवास राव बनाम विनय कुमार एस राव व अन्य, ए० आई० आर० (2004) कर्नाटक 450 के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक द्वारा यदि किसी संयुक्त सम्पत्ति का विक्रय अन्य सदस्यों की सहमति के बिना पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए कर दिया गया हो तो ऐसा अन्तरण शून्यकरणीय होगा जो दूसरे सहदायिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा।
(3) पिता के द्वारा कर्त्ता के रूप में अन्यसंक्रामण – मिताक्षरा विधि में पिता के अधिकार कर्त्ता के रूप में परिवार की सम्पत्ति के निवर्तन के सम्बन्ध में तथाकथित कर्त्ता के अधिकारों से अधिक विस्तृत तथा प्रभावशाली हैं।
वैसे पिता को कर्ता के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उसको कुछ निम्नलिखित विशेष अधिकार सहदायिकी सम्पत्ति के निवर्तन के सम्बन्ध में प्रदान किये गये हैं-
उसे समस्त पैतृक सम्पत्ति को, चाहे चल हो या अचल, बेचने तथा बन्धक रखने का अधिकार प्राप्त है। वह अपने द्वारा लिये गये ऋण की देनगी में अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के हक को निर्तित कर सकता है, यदि ऋण पूर्ववर्ती ऋण है तथा किसी अवैध अथवा अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया।
मधुसूदन बनाम भगवान, (1929) 33 बाम्बे 444 के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने एक बाद में यह निर्णय दिया कि जहाँ पिता ने अपनी आवश्यकता के लिए कुछ रुपया ऋण में लिया और बाद में उसके परिणामस्वरूप संयुक्त सम्पत्ति को बन्धक में दे दिया, यदि यह सिद्ध नहीं होता है कि ऋण अनैतिक उद्देश्य के लिए लिया गया था तो वह बन्धक न केवल पिता के हक को आबद्ध करता है वरन् पुत्रों के भी हक को आबद्ध करता है। पिता निकट सम्बन्धियों को जैसे पुत्री एवं दामाद आदि को स्नेहवश छोटी-छोटी वस्तुओं को दान दे सकता है। परन्तु किसी अनजाने व्यक्ति को अथवा किसी सम्बन्धी को दान देना शून्य होगा। [गुरुममा भत्तार बनाम नगम्मा भत्तार, ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 510
(4) एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक द्वारा अन्यसंक्रामण– एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक सम्पत्ति का अन्यसंक्रामण उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार वह अपनी एकमात्र सम्पत्ति का। उसके द्वारा जीवित दशा में हस्तान्तरण बाद में उत्पन्न हुए पुत्र अथवा दत्तक ग्रहण किये गये पुत्र से अमान्य नहीं हो जाता। किसी इच्छा-पत्र की अवस्था में, यदि उसको कोई पुत्र बाद में उत्पन्न होता है तो वसीयत प्रभावकारी नहीं होगी।
प्रश्न 21. (i) संयुक्त हिन्दू परिवार तथा उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभाजन से आपका क्या तात्पर्य है? विभाजन का दावा कौन कर सकता है? विभाजन का क्या प्रभाव है? कौन-सी सम्पत्ति का विभाजन हो सकता है?
What constitutes a partition in respect of Joint Hindu Family and its property? Who can claim partition? What is the effect of partition? What is the subject-matter of partition?
(ii) हिन्दू विधि के अन्तर्गत विभाजन के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए।
Explain the various modes of partition under Hindu Law.
उत्तर- (i) संयुक्त परिवार सहदायिकी (Joint Family Coparcenary) का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में सहदायिकों (परिवार के सदस्यों) का संयुक्त स्वामित्व (Joint ownership) है। जब तक परिवार संयुक्त है, संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य (सहदायिकी) का सम्पत्ति में विशिष्ट अंश नहीं होता। विभाजन संयुक्त स्वामित्व को तोड़ता है, पृथक् करता है तथा संयुक्त परिवार सम्पत्ति में सहदायिकों का पृथक् अंश सुनिश्चित करता है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सहदायिकी (Coparcener) को विभाजन का दावा करने का अधिकार है।
विभाजन का अर्थ – सम्पूर्ण संयुक्त सम्पत्ति में विभिन्न हितों को व्यवस्थित कर सम्पूर्ण सम्पत्ति के विशिष्ट अंशों का वितरण या विभाजन ही विभाजन या बँटवारा है। मिताक्षरा शाखा के अन्तर्गत विभाजन की परिकल्पना के दो अर्थ हैं –
(1) सम्पूर्ण परिवार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों के विभिन्न अधिकारों के अनुसार उनके विशिष्ट अंशों को व्यवस्थित करना;
(2) संयुक्त परिवार के सदस्यों की संयुक्त स्थिति को इस प्रकार पृथक् करना कि जिससे विधिक परिणाम उत्पन्न होता है।
विभाजन को परिभाषा देते हुए यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में संयुक्त परिवार के सहदायियों (सदस्यों) के अस्थिर (घटते-बढ़ते) हितों को स्थिर करना ही विभाजन है। जैसे ही सहदायिकों या संयुक्त परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार में अंश सुनिश्चित हो जाता है, यह कहा जायेगा कि संयुक्त परिवार में विभाजन हो गया। इस प्रकार विभाजन के पूर्व संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य का अंश या हित स्थिर नहीं रहता। यह बढ़ता घटता रहता है परन्तु एक बार विभाजन (Partition) हो जाने पर संयुक्त परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अंश स्थिर (Crystalize) हो जाता है। विभाजन के पश्चात् पक्षकार चाहें तो भौतिक रूप से विभाजन करवा सकते हैं या सम्पत्ति का संयुक्त उपभोग कर सकते हैं। विभाजन से सहदायिकी का अन्त हो जाता है। विभाजन के लिए अन्य सदस्यों को सहमति या न्यायालय की आज्ञप्ति या लिखित विलेख को आवश्यकता नहीं है। विभाजित होने का एक यह आशय पर्याप्त है जिससे संयुक्त स्थिति में परिवर्तन आता है जब पृथक्ता प्राप्त कर ली जाती है, संयुक्त परिवार की स्थिति विखण्डित हो जाती है।
यदि विभाजित करने योग्य संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं है, विभाजन की घोषणा ही पर्याप्त है। “मैं आपसे (अलग) पृथक् हूँ”-यह घोषणा विभाजन के मस्तिष्क का आशय प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। [गिरधारी लाल बनाम फतेहचन्द, ए० आई० आर० 1955 एम० पी० 148]
विभाजन के लिए सम्पत्ति का अस्तित्व आवश्यक नहीं है। कल्याणी बनाम नारायणन, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 1173 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभाजन के गठन के लिए संयुक्त परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार से पृथक् होने के निश्चित तथा अंसदिग्ध आशय की अभिव्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस आशय की अभिव्यक्ति का प्रारूप (रूपरेखा) क्या होना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह भी आवश्यक है कि इस असंदिग्ध तथा सुनिश्चित आशय का पृथक् होने वाले सदस्यों को ज्ञान (जानकारी) होना आवश्यक है।
कृपा देवी व अन्य बनाम पूनम देवी, ए० आई० आर० (2013) पटना 131, के बाद में न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि यदि संयुक्त परिवार सम्पत्ति का विभाजन सहदायिकों के बीच हो गया हो और प्रत्येक पक्षकार अपने-अपने हिस्से का उपयोग कर रहे हों वहाँ ऐसी सम्पत्ति को दान में देने से किसी पक्षकार को मना नहीं किया जा सकेगा।
विभाजन तथा पारिवारिक व्यवस्था (Partition and Family Arrangement)- विभाजन तथा परिवार की संयुक्त सम्पत्ति के उपभोग की पारिवारिक व्यवस्था में अन्तर किया जाना चाहिए। विभाजन से संयुक्त परिवार की संयुक्त स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संयुक्त परिवार में उसके सदस्यों के अंशों का स्थिरीकरण हो जाता है जबकि पारिवारिक सम्पत्ति के उपभोग की पारिवारिक व्यवस्था से संयुक्त परिवार की संयुक्त स्थिति परिवर्तित नहीं होती। संयुक्त परिवार के सदस्य विभाजन कराये बगैर सहूलियत के लिए संयुक्त सम्पत्ति के समझौते के द्वारा उपभोक्ता के अपने अधिकार सुनिश्चित करा सकते हैं।
पारिवारिक व्यवस्था (Family Arrangement) तथा विभाजन में अग्रलिखित अन्तर है –
पारिवारिक व्यवस्था (Family Arrangement)
(1) पारिवारिक व्यवस्था का उद्देश्य संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में परस्पर विरोधी हितों से सम्बन्धित उचित विवादों को हल करना है।
(2) पारिवारिक व्यवस्था की माँग विधवा C तथा सीमित स्वामी तथा प्रबन्धक (व्यवस्थापक) ऐसे व्यक्तियों से कर सकते हैं जो सहदायिकी नहीं हैं।
(3) पारिवारिक व्यवस्था कभी भी ( एकपक्षीय (Unilateral) नहीं हो सकती।
विभाजन (Partition)
(1) विभाजन परस्पर विरोधी हितों का समझौता नहीं है।
(2) संयुक्त परिवार के सहदायिकी (Coparcener) ही विभाजन की माँग कर सकते हैं।
(3) विभाजन एकपक्षीय (Unilateral) हो सकता है।
विभाजन न करने का करार (Agreement not to partition)- संयुक्त परिवार के सहदायिकों द्वारा संयुक्त परिवार को सम्पत्ति का विभाजन न करने का करार सहदायिकों पर बाध्यकारी नहीं होता अर्थात् यदि किसी सहदायिकों ने संयुक्त परिवार के विभाजन की माँग न करने का करार किया है तो भी वह विभाजन के लिए वाद ला सकता है। काशीनाथ दास बनाम प्रवेश चन्द्र दास, ए० आई० आर० (1978) कलकत्ता 509 नामक बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कई भाइयों ने यह करार किया है कि वे विभाजन की माँग नहीं करेंगे तो उन पर यह करार बाध्यकारी नहीं होगा तथा वे विभाजन के लिए वाद ला सकते हैं क्योंकि ऐसे करार में प्रतिफल का अभाव होता है।
किन सम्पत्तियों का विभाजन हो सकता है? (Properties liable to partition)– सिर्फ सहदायिकी सम्पत्ति हो विभाजन के अधीन है। संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक् (स्वअर्जित) सम्पत्ति विभाजन की विषयवस्तु नहीं हो सकती क्योंकि पृथक् सम्पत्ति इसके स्वामी की आत्यन्तिक सम्पत्ति (Absolute Property) होती है। जिन सम्पत्तियों पर ज्येष्ठाधिकार (Primogeniture) का नियम लागू होता है, वे सम्पत्तियाँ भी विभाजन की विषयवस्तु नहीं हो सकतीं। ज्येष्ठाधिकार नियम के अन्तर्गत पुरखों (पूर्वजों) की सम्पत्ति आती है जिस पर परिवार के ज्येष्ठ सदस्य का अधिकार होता है तथा ऐसी सम्पत्ति के विभाजन की माँग नहीं की जा सकती है। उदाहरण के रूप में राजे, रजवाडे या राज्य पारिवारिक मूर्ति या परिवार का पूजास्थल विभाजन की विषय-वस्तु नहीं है। इसी प्रकार कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका भौतिक रूप में विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे पशु या मेज, कुर्सी आदि के विभाजन की माँग नहीं की जा सकती। ऐसी अविभाज्य सम्पत्ति के विभाजन का तरीका यह है कि इनका मूल्य सुनिश्चित कर लिया जाता है तथा मूल्य को संयुक्त परिवार के सदस्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है या ऐसी अविभाज्य सम्पत्ति का उपभोग संयुक्त परिवार के सदस्य बारी बारी से कर सकते हैं या संयुक्त रूप से सभी सदस्य ऐसी अविभाज्य सम्पत्ति का उपभोग कर सकते हैं।
इस प्रकार संयुक्त परिवार की निम्न सम्पत्तियाँ विभाजन को विषय-वस्तु नहीं हैं, इनके विभाजन की माँग नहीं जा सकती –
(1) अविभाज्य परिसम्पत्ति अर्थात् ऐसी सम्पत्ति जो प्रथा या विधि के किसी प्रावधान या अनुदान की शर्तों के अनुसार परिवार के किसी एक सदस्य को वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है,
(2) ऐसी सम्पत्ति जो अविभाज्य प्रकृति की है। जैसे तालाब, रास्ता या सीढ़ी (Staircase);
(3) पारिवारिक मूर्ति या पुरावशेष (Relics) जो उपासना की विषय वस्तु है;
(4) संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक् सम्पत्ति,
(5) उपासना तथा बलि (Sacrifice) के स्थान या ऐसी सम्पत्ति जो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अर्पित की जा चुकी है,
(6) कुआँ तथा कुएँ से पानी प्राप्त करने का अधिकार तथा
(7) मठाधीश का अधिकार।
विभाजन के पूर्व किये जाने वाले प्रावधान (Provisions to be made before partition)– एक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विभाजन से पूर्व कुछ बातों की पृथक् से व्यवस्था की जानी आवश्यक है –
(1) संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर यदि कोई ऋण बकाया है तो उसके बारे में पृथक् व्यवस्था की जानी चाहिए बशर्ते यह ऋण अनैतिक या अवैध उद्देश्यों के लिए न लिया गया हो;
(2) पिता का व्यक्तिगत ऋण बशर्ते यह ऋण अनैतिक तथा अवैध उद्देश्य के लिए न हो;
(3) अहं (Qualified) वारिसों (Heirs) या सम्भावित उत्तराधिकारियों तथा परिवार की महिला सदस्यों के भरण-पोषण के लिए पृथक् व्यवस्था;
(4) संयुक्त हिन्दू परिवार के अन्तिम पुरुष सदस्य (धारक) की अविवाहिता पुत्री के विवाह के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था [शंकर बनाम प्रशासनिक प्रापक, ए० आई० आर० 1977 मद्रास 171]
(5) अन्तिम पुरुष धारक (Last male holder) की माता तथा विधवा के अन्तिम संस्कार के लिए आवश्यक व्यय ।
यदि किसी सदस्य के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए कोई पृथक् तथा अतिरिक्त प्रभार (Charge) की व्यवस्था की जाये।
संक्षेप में कहा जाये तो संयुक्त हिन्दू परिवार के विभाजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय हैं –
(1) विभाजन के पृथक् तथा स्पष्ट आशय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए,
(2) संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पत्ति की नाप-तौल कर विभाजन किया जाना आवश्यक नहीं है;
(3) विभाजन या पृथक् होने का कारण दिया जाना आवश्यक नहीं है;
(4) संयुक्त परिवार में वयस्कों की उपस्थिति विभाजन में रुकावट (अड़चन) नहीं है।
विभाजन की माँग कौन कर सकता है? (Who can demand partition ) – संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विभाजन की माँग निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते –
(1) विधवा (Widow)- मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत विधवा संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक (Coparcener) नहीं मानी जाती तथा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के विभाजन की माँग सिर्फ सहदायिक (Coparcener) ही कर सकते हैं परन्तु हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के कारण हिन्दू विधवा को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के विभाजन की माँग करने का अधिकार है। दो विधवाओं के मध्य परिसम्पत्ति का विभाजन दूसरे को आवंटित सम्पत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार को नष्ट नहीं करता। एक पक्षकार यदि यह कहता है कि पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत उसने उत्तराधिकार के अपने अधिकार को छोड़ दिया था तो उसे यह तथ्य ठोस सबूतों द्वारा साबित करना होगा।
(2) पुत्र या पौत्र (Son or Grand Son)- मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत एक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा सहदायिकी के प्रत्येक वयस्क सदस्य को अन्य सदस्यों की सहमति के विरुद्ध भी विभाजन की माँग करने का अधिकार है। बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विचार व्यक्त किया कि पिता के जीवन काल में पिता की अनुमति (सहमति) के बिना संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन की माँग करने का अधिकार पुत्र को नहीं है, जब पिता अपने पिता, भाई तथा भतीजों से पहले से ही पृथक् नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने पुत्तो रंगम्मा बनाम रंगम्मा (ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 1018) नामक बाद में यह विचार प्रकट किया कि संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति के विभाजन के लिए बाद किसी सहदायिकी द्वारा लाया जा सकता है (पोषणीय है) भले ही पिता अपने भाई से पृथक् नहीं हुआ है तथा पिता विभाजन के लिए इच्छुक नहीं है या विभाजन के लिए सहमति नहीं देता है। इस मत का समर्थन बम्बई उच्च न्यायालय ने डॉ० नीलकन्था बनाम डॉ० रामचन्द्र, ए० आई० आर० 1991 बम्बई 10 नामक बाद में किया है।
(3) अधर्मज या अवैध पुत्र (Illegitimate Son)- एक अधर्मज या अवैध (Illegal) पुत्र संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में कोई हित नहीं रखता तथा उसे सहदायिकी संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन की माँग करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि उसे अपने पिता की परिसम्पत्ति से भरण-पोषण की माँग करने का अधिकार है। मद्रास तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया कि एक शूद्र के अवैध या अधर्मज पुत्र को अपने अधर्मज भाइयों के साथ विभाजन लागू कराने का अधिकार है परन्तु वह अपने पिता या अपने पिता के सहदायिकों के विरुद्ध विभाजन लागू नहीं करा सकता। बम्बई उच्च न्यायालय ने भी इस विचार का समर्थन किया है परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपरीत विचार प्रकट किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया है कि विभाजन के बाद के दाखिल होने के पश्चात् पिता अपने अधर्मज पुत्र का अंश (Share) निश्चित कर सकता है। वह अपने इस अधिकार का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार तब तक कर सकता है जब तक विभाजन अन्तिम अधिकार न हो जाय। [(1955) 1 एम० एल० जे० 120]
(4) दत्तक पुत्र (Adopted son)- दत्तक ग्रहण करने के पश्चात् एक दत्तक पुत्र को विभाजन की माँग करने का अधिकार प्राकृतिक पुत्र (Natural son) की भाँति है परन्तु यदि एक माता-पिता ने पुत्र को दत्तक लिया है तथा उसके पश्चात् उन्हें पुत्र का जन्म हो जाता है, यद्यपि दत्तक पुत्र का अधिकार पत्नी या प्राकृतिक पुत्र के समान ही होगा। परन्तु संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में उसके अंश का निर्धारण भिन्न-भिन्न शाखा (Schools) में भिन्न-भिन्न होगा। बंगाल में वह 1/3 अंश पाएगा, बनारस शाखा में वह संयुक्त परिवार सम्पत्ति का 1/4 अंश पायेगा तथा बम्बई तथा मद्रास में वह 1/5 अंश पायेगा। हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ने इस विभेद को समाप्त कर दिया है तथा दत्तक पुत्र को विभाजन होने पर संयुक्त परिवार सम्पत्ति में प्राकृतिक पुत्र के समान अंश प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया है।
(5) पश्चात् उत्पन्न पुत्र (After born sons)— विभाजन के सम्बन्ध में पश्चात् उत्पन्न पुत्रों को दो भागों में बाँटा जा सकता है
(1) वे पुत्र जो विभाजन के पश्चात् गर्भ में आये तथा जिन्होंने विभाजन के पश्चात् जन्म लिया,
(2) दूसरे वे पुत्र जो विभाजन के पूर्व गर्भ में आये थे परन्तु जिनका जन्म विभाजन के पश्चात् हुआ हो।
एक ऐसा पुत्र जो माता के गर्भ में आ गया है, हिन्दू विधि के अनुसार उसका अस्तित्व संसार में मान लिया जाता है। अतः यदि एक पुत्र विभाजन के पूर्व गर्भ में आ गया है तथा विभाजन के पश्चात् जन्म लेता है, उसे अपने जन्म के पूर्व विभाजन को पुनः खोलवाने (Re open) का अधिकार है तथा उसे संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अपने अन्य भाइयों के समान अंश प्राप्त होगा।
यदि एक पुत्र विभाजन के पश्चात् गर्भ में आया है तथा विभाजन के पश्चात् उत्पन्न हुआ है तथा पिता, विभाजन में अपने अंश को प्राप्त कर अन्य पुत्र से पृथक् हो गया है तो ऐसा पश्चात्वर्ती उत्पन्न पुत्र विभाजन पर अपने पिता को प्राप्त अंश प्राप्त करने का अधिकारी है। यद्यपि उसे विभाजन को पुनः खुलवाने का अधिकार नहीं है परन्तु वह पृथक् हुए पुत्रों को अपवर्जित कर अपने पिता की पृथक् सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है।
(6) अवयस्क सहदायिक (Minor Coparcener)– यदि संयुक्त परिवार में उसकी संयुक्त स्थिति उसके हित में लाभप्रद नहीं रहती तो अवयस्क सहदायिक (Minor Coparcener) संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में विभाजन की माँग कर सकता है। चूँकि एक अवयस्क विभाजन के लिए वाद नहीं ला सकता है अतः कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ओर से विभाजन के लिए वाद दाखिल कर सकता है। किसी व्यक्ति का अवयस्क होना विभाजन के मार्ग में अड़चन नहीं बन सकता। यदि विभाजन किसी अवयस्क के हितों के विपरीत है तो अवयस्क वयस्कता प्राप्त करने पर विभाजन को चुनौती दे सकता है।
(7) अन्तरिती (Alience) – अन्तरिती वह व्यक्ति है जिसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति या उस सम्पत्ति में कोई हित हस्तान्तरित किया गया है। संयुक्त परिवार के सहदायिकी के किसी हित के अन्तरिती को, यदि हस्तान्तरण वैध है तो उसे विभाजन की माँग करने का अधिकार है।
श्रीमती कैलाशपति देवी बनाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, आई० आर० 1984 एस० सी० 1802 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य से सम्पत्ति के क्रेता को संयुक्त परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाजन के लिए।
सामान्य वाद लाने का अधिकार है। बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालयों के अनुसार किसा ऋण की वसूली की आज्ञाप्ति के निष्पादन में भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार ऐसे आज्ञप्तिधारी को है।
(8) महिला अंशधारी (Female Sharer) — संयुक्त हिन्दू परिवार के सन्दर्भ में महिला अंशधारियों में निम्न महिलाएँ आती हैं –
(1) पत्नी:
(2) विधवा माँ एवं
(3) पैतृक मातामही (दादी) (Paternal-Grandmother)
यद्यपि महिला अंशधारियों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में विभाजन की माँग करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि संयुक्त परिवार को विभाजित सम्पत्ति में उन्हें अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार है, जहाँ एक सहदायिकी द्वारा विभाजन का वाद दाखिल किया गया तथा वाद वापस ले लिया गया है, महिला अंशधारक वाद को चालू नहीं रख सकती तथा अपने अंश को माँग नहीं कर सकती। यदि विभाजन का वाद किसी कारण खारिज हो जाता है, सम्पत्ति में विभाजन की माँग माता द्वारा नहीं की जा सकती। [बलदेव बनाम सरोजिनी, 34 कम्पनी वीकली नोट्स 1601]
विभाजन पर माता तथा दादी तभी अपने अंशों को माँग कर सकती हैं, जब पुत्रों तथा पौत्रों के मध्य विभाजन प्रभावी हो गया है। महिला अंशधारक संयुक्त सम्पत्ति में अपने अंशों पर अधिकार सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं कर सकती है कि विभाजन के लिए वाद दाखिल कर दिया गया है या किसी वाद में प्राथमिक आज्ञप्ति पारित कर दी गई है। दूसरे शब्दों में वाद दाखिल कर देने मात्र से या बाद में प्राथमिक आज्ञप्ति पारित हो जाने मात्र से महिला अंशधारक संयुक्त सम्पत्ति में अपने अंश की माँग नहीं कर सकती। संक्षेप में जब तक वास्तविक विभाजन नहीं हो जाता, महिला अंशधारकों को संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अंशों का आवंटन सम्भव नहीं है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 महिला उत्तराधिकारियों के निवास स्थान गृहों में विभाजन का दावा करने के अधिकार को तब तक स्थगित रखती है जब तक संयुक्त परिवार के पुरुष उत्तराधिकारी अपने अंशों को विभाजित करने के विकल्प का चुनाव नहीं कर लेते।
विभाजन का प्रभाव (Effect of Partition)- विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि विभाजन से संयुक्त स्थिति विखण्डित हो जाती है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी का अन्त हो जाता है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक सहदायिकों का संयुक्त परिवार में अंश सुनिश्चित हो जाता है। विभाजन का निम्न प्रभाव होता है –
(1) सामान्य विभाजन के पश्चात् अविभाजित परिवार की इकाई समाप्त हो जाती है जहाँ विभाजन आंशिक है जो सदस्य इकाई से पृथक् हो गये हैं उनकी संयुक्त स्थिति समाप्त हो जाती है,
(2) यदि विभाजन धर्म परिवर्तन (Conversion) के कारण होता है, सम्परिवर्तित (Convers) का परिवार के अन्य सदस्यों से सम्बन्ध पृथक् हो जाता है। यदि विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह के कारण विभाजन होता है। विवाह करने वाले सहदायिक से परिवार के अन्य सदस्यों का सम्बन्ध पृथक हो जाता है;
(3) विभाजन स्वयं के परिवार तथा सहदायिकी के चरित्र को परिवर्तित कर देता है। मिताक्षरा को ज्ञात संयुक्त काश्तकारी (Joint tenancy) सहदायिकी की सहकाश्तकारी (Tenancy-in-common) में परिवर्तित हो जाती है,
(4) विभाजन परिवार तथा अन्य सम्बन्धों को समाप्त नहीं करता परन्तु उससे सम्बन्धित अन्य सम्बन्ध यथावत् रहते हैं। जैसे-उत्तराधिकार का अधिकार एक बार विभाजन साबित कर दिया जाता है तो संयुक्त केन्द्रक (Joint Nucleus) नहीं रह जाता तथा संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम, सम्पत्ति की प्राप्ति का प्रश्न नहीं रह जाता।
उत्तर- (ii) हिन्दू विधि के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि विभाजन एक रजिस्टर्ड प्रलेख द्वारा निष्पन्न किया जाय। कोई एक पारिवारिक समझौता सहदायिकों के बीच विभाजन कराने के लिए पर्याप्त है और उससे उनको पृथक् अंश का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसका वे उपभोग कर सकते हैं। कोई भी विभाजन (1) पिता द्वारा अपने जीवन काल में अपने तथा अपने पुत्रों के बीच सम्पन्न किया जा सकता है; अथवा (2) आपसी समझौते के द्वारा अथवा (3) वाद दायर करके अथवा (4) परस्पर विवाचन द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। 1 विभाजन के लिए यह जरूरी नहीं है कि सम्पत्ति टुकड़े-टुकड़े में विभाजित हो । प्रास्थिति में परिवर्तन उपर्युक्त किसी भी एक तरीके से लाया जा सकता है और कुछ सम्पत्तियाँ वे साथ साथ सह-आभोगी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
(1) केवल घोषणा द्वारा विभाजन- चूँकि मिताक्षरा के अनुसार बँटवारा संयुक्त स्तर को समाप्त करता है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत इच्छा का विषय है। अतएव बँटवारा के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि सदस्य द्वारा स्पष्ट रूप से उसके लिए “इच्छा” प्रकट की जाय कि वह संयुक्त परिवार से पृथक् होकर पृथक्ता से अपने भाग का उपभोग करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने रघवम्मा बनाम चेन्चेम्मा, ए० आई० आर० (1964) एस० सी० 136 के बाद में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि बँटवारे के सम्बन्ध में न केवल एकतरफा इच्छा की घोषणा पर्याप्त नहीं है, यह भी आवश्यक है कि इस इच्छा की घोषणा की जानकारी उन सभी लोगों को अवश्य संचारित की जाय जो उससे प्रभावित हो रहे हों। हवा में की गई बँटवारे की घोषणा कोई घोषणा नहीं है।
पृथक्करण (विभाजन) की इच्छा की घोषणा अन्य सहदायिकों तक अवश्य पहुँचनी चाहिए, चाहे जैसे भी पहुँचे। इस नियम को उच्चतम न्यायालय ने पुत्तारे गम्मा बनाम एम० एस० रेगन्ना, ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 1618 के बाद में जोरदार शब्दों में प्रतिपादित किया।
(2) नोटिस द्वारा बँटवारा – संयुक्त स्थिति को समाप्त करने के लिए अन्य सहदायिक को नोटिस देकर भी बँटवारा किया जा सकता है। उस नोटिस में पृथक् होने की इच्छा और बँटवारा की माँग होनी चाहिए। नोटिस बाद में अन्य सहदायिकों की राय से वापस भी ली जा सकती है और यदि नोटिस वापस ले ली जाती है तो यह समझा जायेगा कि बँटवारा नहीं होगा।
(3) अन्य जाति में परिवर्तन- जब एक सहभागीदार अपना धर्म परित्याग करके अन्य धर्म अपना लेता है तो उसमें तथा अन्य सहदायिकों की संयुक्त स्थिति में बँटवारा हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तित व्यक्ति द्वारा उत्तरजीविता द्वारा सम्पत्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि परिवर्तन के समय से ही वह व्यक्ति सहदायिक नहीं रह जाता तथा वह परिवर्तित होने की स्थिति के अनुसार, अंश पाने का अधिकारी होता है।
(4) विशेष-विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अन्तर्धार्मिक विवाह करने से भी अन्य सहदायिकों में बँटवारा हो जाता है।
(5) वाद दायर कर– बँटवारे का वाद दायर करने से भी शीघ्र बँटवारा हो जाता है। बादी के अंश पृथक् होने के अधिकार का व्यक्तिकरण ही संयुक्त सम्पत्ति से उसकी पृथक् स्थिति का द्योतक है, चाहे वह परिणामतः विनिश्चय प्राप्त करे अथवा नहीं।
(6) सहमति से बँटवारा– जब संयुक्त परिवार के सदस्य आपस में यह निश्चित करते हैं या चाहते हैं कि वह पृथक्-पृथक् स्वामी हों और बँटवारे के लिए सहमत होते हैं तो प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निश्चित करके बँटवारा किया जा सकता है। यद्यपि यह बँटवारा अलग-अलग हिस्सा नहीं होता है। [ अप्रूवियम बनाम रावसुब्बा अय्यर, 11 एम० आई० ए० 75 (पी०सी०) ]
मेजर प्रेमनाथ बनाम राजिन्दर नाथ, ए० आई० आर० 1986, दिल्ली 121 के बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त परिवार की विभिन्न शाखाओं के मुखिया अपने अंशों को आपसी सहमति से निर्धारित कर लेते हैं तो इससे यह मान लिया जायेगा कि संयुक्त पिरवार की सम्पत्ति में विभाजन हो गया, भले ही इसका सीमांकन व माप बाद में ही किया जाय।
(7) विवाचन द्वारा बँटवारा – जब परिवार के सदस्य किसी मध्यस्थ को बुलाकर बँटवारा करना चाहते हैं तो उसे विवाचन द्वारा बँटवारा कहते हैं। केवल पंचनिर्णय न देने से प्रमाणित नहीं होता है कि पृथक् होने की नीयत ही छोड़ दी गयी है।
(8) पिता द्वारा बँटवारा- पिता बिना अपने पुत्रों की सलाह लिए बँटवारा कर सकता। है। यह प्राचीन सिद्धान्तों में व्यक्त पिता का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय कल्याणी बनाम नारायणन, ए० आई० आर० (1980) एस० सी० 1173 के अनुसार एक हिन्दू पिता अपने पुत्रों के साथ मिताक्षरा विधि के अधीन संयुक्त परिवार के प्रबन्धक को मौजूदगी में भी विभाजन करवा सकता है तथा पुत्रों को बाधित कर सकता है। इसके द्वारा वह पुत्रों को अपना अंश निर्धारित करके उनको अलग कर सकता है किन्तु उसको संयुक्त परिवार की सम्पत्ति परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच इच्छापत्र के माध्यम से विभाजित करने का अधिकार नहीं है। वह भले ही उनकी सहमति से इस प्रकार कर सकता है।
उपर्युक्त विभाजन की आठ विधियाँ सर्वांगपूर्ण नहीं हैं। इसके अन्तर्गत कोई भी स्थिति, जिससे विभाजन का मत प्रदर्शन होता हो, आ सकती है।
प्रश्न 22. “एक बार किये गये विभाजन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है।” इस नियम को समझाइये तथा इसके अपवादों का वर्णन कीजिये।
“Partition once made cannot be reopened.” Explain this rule and point out its exceptions.
उत्तर- एक बार किये गये विभाजन पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है – मनु का कथन है कि विभाजन एक बार होता है, पुत्री एक चार विवाह में दो जाता है तथा “मैं देता हूँ” मनुष्य एक बार कहता है ये तीनों वस्तुएँ सुयोग्य व्यक्ति से एक बार सदैव के लिए तथा अप्रतिसंहरित रूप से करते हैं।
एक बार किये गये विभाजन पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। जब परिवार में विभाजन हो जाता है तो संयुक्त प्रास्थिति टूट जाती है, भले ही विभाजन ऋणदाताओं के हक को समाप्त करने के लिए किया गया हो। यदि विभाजन दाखिल खारिज से प्रमाणित हो जाता है तो वह अन्तिम होगा. भले ही वह दूरस्थ उद्देश्य से किया गया हो। ऐसा विभाजन परिवार के उन सदस्यों पर बाध्यकर होगा जो विभाजन के पूर्व संयुक्त थे।
एस० नायक बनाम सत्यवादी नायक, ए० आई० आर० (1984) उड़ीसा 30 के मामले में 1918 में विभाजन हो जाने के बाद सिफ इस बात पर कि परिवार के किसी एक व्यक्ति को दशकों बाद विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. पुनः विभाजन नहीं करवाया जा सकता। विभाजन संयुक्त स्थिति (सहदायिकी) को भंग कर देता है। हितों की सामूहिकता समाप्त हो जाती है। विभाजन के बाद सम्पत्ति पाने पर सदस्यों को वह पृथक सम्पत्ति हो जाती हैं। पुनः विभाजन तभी सम्भव है यदि पूर्व विभाजन के बाद पुरुष सदस्यों ने अपनी-अपनी सम्पत्ति का पुनः एकीकृत होने के इरादे से विलयन कर दिया हो l
अपवाद उक्त सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं तथा निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजन पर पुनर्विचार किया जा सकता है –
(1) पुत्र जो विभाजन के समय उत्पन्न न हुआ हो, परन्तु गर्भ में आ गया हो, विभाजन पर पुनर्विचार करवा सकता है यदि उसके लिए अंश सुरक्षित नहीं रखा गया हो। दूसरी तरफ यदि कोई पुत्र विभाजन के बाद ही गर्भ में आया हो तथा उत्पन्न हुआ हो तथा उसके पिता का अंश मिल चुका हो तो वह विभाजन पर पुनर्विचार नहीं करवा सकता। वह केवल पिता की मृत्यु के पश्चात् उसके अंश का तथा अपनी स्वार्जित सम्पत्ति का भागी होगा।
(2) वह पुत्र जो विभाजन के पश्चात् ही गर्भ में आया हो तथा उत्पन्न हुआ हो, विभाजन पर पुनर्विचार करवा सकता है, यदि उसके पिता को विभाजन में अंश का अधिकार होते हुए भी कोई अंश न मिल पाया हो।
(3) कोई अनहींकृत सहदायिक अनर्हता की समाप्ति पर तथा किसी खोये हुए सहदायिक के लौट आने पर विभाजन पर पुनर्विचार करवा सकता है।
(4) कोई अवयस्क सहदायिक होने पर विभाजन पर पुनर्विचार करवा सकता है। यदि उसके अवयस्क रहने की अवस्था में किया गया विभाजन अनुचित अथवा उसके हितों के विपरीत हो। उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती सुखरानी बनाम हरीशंकर, ए० आई० आर० (1979) एम० सी० 1430 के मामले में यह
अभिनिर्धारित किया है कि यदि विभाजन अवयस्क के हितों के विरुद्ध अथवा अनुचित रूप से हुआ है तो वयस्क द्वारा विभाजन पर पुनः विचार करवाया जा सकता है, भले ही विभाजन में किसी प्रकार का कपट, मिथ्या व्यपदेशन (misrepresentation) तथा अनुचित प्रभाव (Undue influence) प्रभावी न हुआ हो।
(5) इसी प्रकार यदि किसी सहदायिक ने विभाजन में कोई अनुचित भाग प्रदान कर लिया हो तो विभाजन का पुनर्समायोजन हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने रतनम चेट्टियार बनाम एस० एम० कुटरुस्वामी, ए० आई० आर० (1979) एस० सी० के बाद में यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सदस्य की स्वेच्छा से अथवा सहमति से यदि विभाजन होता है तो तब तक पुनः विचारित नहीं हो सकता जब तक यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि विभाजन धोखा देकर, दबाव में गलत प्रतिनिधित्व करके अथवा अनुचित प्रभाव डाल करके प्राप्त किया गया था।
जहाँ संयुक्त परिवार में अवयस्क होते हैं तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि विभाजन अनुचित तथा न्यायोत्तर है तथा अवयस्कों के हित के विरुद्ध है, वहाँ विभाजन पर पुनः विचार किया जा सकता है।
प्रश्न 23 (i) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने की पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा मुख्य लक्षणों की चर्चा करें। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार विधि में क्या मुख्य परिवर्तन किये गये?
Write down the history, object and main features and the changes brought out by the Hindu Succession Act, 1956.
(ii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के सम्बन्ध में संशोधित अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत क्या परिवर्तन लाये गये। क्या ये पुत्र एवं पुत्रियों के बीच के ( सम्पत्ति सम्बन्धी) विभेद को समाप्त करते हैं?
उत्तर- (i) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, 17 जून, 1956 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा हिन्दुओं के निर्वसीयती उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों में विस्तृत तथा ठोस परिवर्तन किये गये ये परिवर्तन हिन्दू समाज के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तन के अनुरूप थे। काफी समय से यह माँग की जाती रही है कि उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू महिलाओं को हिन्दू पुरुषों के समान अधिकार दिया जाय। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने इस माँग को काफी सीमा तक पूरा किया।
सन् 1937 में हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम (Hindu Women’s Right to Property Act) पारित हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् सरकार ने विधि की इस शाखा में सुधार या संशोधन का सुझाव देने के लिए राव समिति को स्थापना की। राव समिति ने हिन्दू उत्तराधिकार के तत्कालीन विद्यमान नियमों का विस्तृत अध्ययन किया। इस समिति ने हिन्दू उत्तराधिकार के तात्कालिक नियमों में महिलाओं के साथ बरती जा रही असमानता तथा अन्याय को समाप्त करने के प्रयोजन से क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। इस समिति ने हिन्दू उत्तराधिकार से सम्बन्धित नियमों के संहिताकरण की संस्तुति की।
राव समिति की संस्तुति पर विधायिका द्वारा कई विधेयक पारित किये गये। इन विधेयकों ने जिन अधिनियमों का रूप लिया, उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 प्रमुख है।
उद्देश्य – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 प्रगतिशील समाज को आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पारित किया गया। पुरानी विधि तत्कालीन गतिशील हिन्दू समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम थी यद्यपि विभिन्न विधायी संशोधनों तथा न्यायिक निर्णयों ने इसमें कुछ परिवर्तन किये थे। हिन्दू समाज के सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाली समान विधि की आवश्यकता को भी यह अधिनियम काफी हद तक पूरा करता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हिन्दू समाज के पुरुषों तथा महिलाओं के मध्य उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विद्यमान असमानताओं को दूर करता है। निर्वसीयत उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यह अधिनियम वारिसों को एक सूची प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम उत्तराधिकार की सम्पूर्ण विधि को संशोधित या संहिताबद्ध करने के प्रयोजन से पारित किया गया।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रमुख लक्षण (Main Characteristics of Hindu Succession Act, 1956)–(1) यह अधिनियम भारतवर्ष के सभी हिन्दुओं के लिए समान (एक रूप) उत्तराधिकार के लिए नियमों को प्रतिपादित करता है चाहे वे उत्तर भारत के मिताक्षरा शाखा से या पूर्व में बंगाल के दायभाग या दक्षिण भारत के मरूमक्कट्टायम, अलियसान्धना तथा नम्बूदरी शाखा से शासित हों। यह अधिनियम सभी हिन्दुओं पर लागू होता है तथा हिन्दू में बौद्ध, जैन तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं (धारा 2)। यह अधिनियम उस व्यक्ति की सम्पत्ति पर लागू नहीं होता जिस पर विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं (धारा 5) ।
(2) यह अधिनियम हिन्दुओं के उत्तराधिकार से सम्बन्धित सभी नियमों को निरुद्ध करता है चाहे ऐसे नियम हिन्दू पुस्तकों, प्रथा या ऐसी रीति रिवाजों में निहित हों जिनका विधिक प्रभाव हो। यदि राज्य या केन्द्रीय विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम के प्रतिकूल हैं या विरोधाभासी हैं तो इस अधिनियम (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956) का नियम ही प्रभावी होगा।
(3) यह अधिनियम अविभाज्य सम्पदा (Impartible Estate) तथा इसके उत्तराधिकार की विधि को समाप्त करता है।
(4) यह अधिनियम हिन्दू महिलाओं के सीमित परिसम्पत्ति (सम्पदा) को समाप्त करता है। यह अधिनियम हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति या सम्पदा का पूर्ण स्वामी बनाता है। चाहे सम्पत्ति किसी भी स्रोत से आयी हो तथा वह ऐसी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार जैसे भी चाहे, निस्तारित, हस्तान्तरित या अन्तरित कर सकती है (धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956)।
(5) यह अधिनियम हिन्दू महिला की सम्पत्ति में एक समान उत्तराधिकार का क्रम निर्धारित करता है। यदि एक महिला निर्वसीयत मरती है तो उसकी सम्पत्ति उसके बच्चों तथा उसके पति में न्यागत होगी अर्थात् उसके बच्चों तथा पति को मिलेगी। बच्चों तथा पति के अभाव में महिला की सम्पत्ति उसके माता-पिता तथा माता-पिता के वारिसों (उत्तराधिकारियों) को प्राप्त होगी। यदि महिला सन्तानहीन मरती है तथा उसने कोई वसीयत नहीं की है तो उसके माता-पिता से महिला को प्राप्त सम्पत्ति उसके पति या उसके पति के उत्तराधिकारियों को प्राप्त न होकर उसके माता-पिता के उत्तराधिकारियों पर पुनः वापस आ जायेगी।
अपने माता-पिता से या किसी भी स्रोत से राधा एक सम्पत्ति प्राप्त करती है तथा उसकी पूर्ण स्वामिनी बन जाती है। यदि राधा निर्वसीयत मरती है तो उसकी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके निर्वसीयत मरने पर उसके बच्चों तथा उसके पति पर न्यागत (devolve) होगी। उसके सन्तानहीन होने पर सम्पत्ति यदि उसके माता-पिता से प्राप्त है तो उसकी सम्पत्ति उसके माता-पिता तथा उनके उत्तराधिकारियों को वापस प्राप्त हो जायेगी। वह सम्पत्ति उसके बच्चों या पति के वारिसों को प्राप्त नहीं होगी।
(6) यदि कोई बच्चा गर्भ में आ गया है तथा जीवित जन्म लेता है तथा बच्चे का जन्म निर्वसीयती व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् होता है तो उस बच्चे का उत्तराधिकार निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु की तिथि तक वापस निहित हो जायेगा। (धारा 20)
(7) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रतिपादित करता है कि पुरुष या महिला निर्वसीयती के पूर्ण रक्त सम्बन्धी उत्तराधिकारियों को अर्द्ध रक्त सम्बन्धी उत्तराधिकारियों पर उत्तराधिकार में वरीयता प्राप्त होगी। (धारा 18)
दूसरा नियम यह है कि यदि निर्वसीयत सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले वारिस दो या दो से अधिक होते हैं तो वे अपना अंश प्रति व्यक्ति न कि प्रति पट्टी (They will inherit per capita not per strips) प्राप्त करेंगे। ऐसे वारिस सम्पत्ति को सामान्य आसामी (Tenant in-common) की भाँति प्राप्त करेंगे संयुक्त आसामी (Joint Tenant) की भाँति नहीं।
(8) इस अधिनियम ने उत्तराधिकार से अपवर्जित किये जाने के नियम को पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 28 ने शारीरिक त्रुटियों, शारीरिक अपंगता या शारीरिक रोग पर आधारित, सभी आधारों का अपवर्जन कर दिया है। अनर्हता (अयोग्यता)
(Disqualification) सिर्फ निम्न पर लागू होगी अर्थात् निम्न व्यक्ति उत्तराधिकार से अयोग्य (अनर्ह) (Disqualified) होंगे –
(1) पूर्व मृत पुत्र की विधवा यदि उसने पुनर्विवाह कर लिया है।
(2) पूर्व मृत पुत्र के पूर्व पुत्र की विधवा।
A ————- B –‐——– C
पूर्व मृत पुत्र —- B का पूर्व मृत पुत्र —- उसकी विधवा
(3) भाई की विधवा
(4) मृतक का हत्यारा जो साम्या तथा न्याय के सिद्धान्त पर उत्तराधिकार से अपवर्जित होता है।
यदि किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन (Conversion) कर लिया है तो उसे उत्तराधिकार से अपवर्जित नहीं किया गया है परन्तु धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के वंशज अपने हिन्दू सम्बन्धियों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से अपवर्जित किये गये हैं।
(9) एक अवैध अधर्मज (Illegitimate) पुत्र के अपनी माता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार को तो सुरक्षित रखा गया है परन्तु एक अवैध या अधर्मज पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से अपवर्जित कर दिया गया है।
(10) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्तराधिकार सामान्य रूप से को निकटता (Propinquity) पर आधारित है। रक्त की निकटता के आधार इस अधिनियम ने उत्तराधिकारियों को तीन की अपेक्षा चार वर्गों में विभाजित किया है।
ये चार उत्तराधिकारी निम्न हैं –
(1) अनुसूची के प्रथम वर्ग के वारिस उत्तराधिकारी (Heirs of Class I of Schedule)
(ii) अनुसूची के द्वितीय वर्ग के वारिस या उत्तराधिकारी (Heirs of Class It of Schedule)
(iii) पितृबन्धु गोत्रज गोती (Agnates)
(iv) मातृबन्धु या बन्धु (Cognates)।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची में उत्तराधिकारियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सम्पत्ति सर्वप्रथम उत्तराधिकारी के प्रथम वर्ग के वारिसों, उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। प्रथम वर्ग में सोलह (2005 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा अन्त:स्थापित) वरीयता प्राप्त वारिसों या उत्तराधिकारियों का उल्लेख है। यदि प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों में से कोई भी नहीं है तो सम्पत्ति द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के उत्तराधिकारियों को इस अधिनियम की धारा 8 व 9 में निर्धारित क्रम में प्राप्त होगी। उपरोक्त विभाजन का प्रमुख लक्षण यह है कि प्रथम वर्ग के वारिस सम्पत्ति एक साथ (Simultaneously) उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के मामले में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त भी लागू होता है।
दूसरा उल्लेखनीय लक्षण यह है कि अनुसूची के प्रथम वर्ग के वारियों या उत्तराधिकारियों में उल्लिखित सोलह वारिसों में से ग्यारह महिलाएँ हैं तथा पाँच पुरुष वारिस हैं। इन पाँच पुरष वारिसों (Male heirs) में से एक महिला के माध्यम से दावा करता है। वर्ग एक में उल्लिखित सभी बारह वारिस (Heirs) एक साथ तथा समान अंश में सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। (2005 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा अन्तःस्थापित) द्वितीय वर्ग (Class-II) में उल्लिखित सभी व्यक्ति एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करते परन्तु प्रथम प्रविष्टि (First Entry) में उल्लिखित व्यक्ति एक साथ (साथ-साथ Simultaneously) उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के वारिस उत्तराधिकारी अर्थात् पितृबन्धु एवं मातृबन्धु या बन्धु के वरीयता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।
(II) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने मिताक्षरा सहदायिकी को सम्पूर्ण परिकल्पना को प्रभावित किया है। मिताक्षरा सहदायिकी की परिकल्पना उत्तरजीविता (Survivorship) के नियमों से शासित होती थी। उत्तरजीविता के नियमों के अनुसार, संयुक्त सम्पत्ति में सहदायिकों का हित विभाजन तक स्थिर नहीं होता। यह दोलायमान अर्थात् घटता बढ़ता रहता है। यदि कोई सहदायिक विभाजन के पूर्व मर जाता है तो अन्य सहदायिकों के अंश में वृद्धि होती है तथा यदि संयुक्त परिवार में किसी सहदायिकी का जन्म होता है तो संयुक्त परिवार में अन्य सहदायिकों का अंश घट जाता है। मिताक्षरा सहदायिकी परिकल्पना में महिलाओं को संयुक्त परिवार में कोई हित प्राप्त नहीं था। वे विभाजन को माँग नहीं कर सकती थीं। उन्हें भरण-पोषण तक का सोमित अधिकार था। उन्हें सम्पत्ति के अनतरण का अधिकार नहीं था। अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरजीविता (Survivorship) के नियमों का प्रयोग अति सीमित है। अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरजीविता के नियम वहीं लागू होते हैं जहाँ सहदायिकों का पुरुष सदस्य अपने पीछे सिर्फ सहदायिकों को छोड़कर मरता है।
यदि मिताक्षरा सहदायिकी का पुरुष सदस्य वर्ग एक में उल्लिखित स्त्री या महिला वारिस (उत्तराधिकारी) छोड़कर मरता है तब मृतक की सम्पत्ति उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत नहीं होगी परन्तु मृतक की सम्पत्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यागत (devolve) होगी। यह अधिनियम महिला वारिस को विशिष्ट अंश प्रदान करता है। अब हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के पश्चात् एक सहदायिकी के रूप में पुत्री भी होगी।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उल्लिखित कुछ शब्दावली
(1) वारिस या उत्तराधिकारी (Heirs)- मृत व्यक्ति की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाला व्यक्ति वारिस या उत्तराधिकारी कहलाता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3 (क) के अनुसार, वारिस से तात्पर्य ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो निर्वसीयत को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अन्तर्गत हकदार है।
(2) वंशज (Descendant)–किसी व्यक्ति की सन्तान उस व्यक्ति की वंशज है। किसी व्यक्ति के पुत्र तथा पुत्री उसके निकटतम वंशज हैं। पुत्र तथा पुत्री के पश्चात् पुत्र तथा पुत्री की सन्ताने तथा उनकी सन्तानें तथा किन्हीं भी निचली डिग्री के उसके नातेदार उसके वंशज (descendant) कहलाते हैं।
क
पुत्र पुत्री नानी पितामह
पौत्र दोहती |की वंशज |का वंशज
प्रपौत्र परदोहती माता पिता
(3) पूर्वज (Ascendant)– किसी भी व्यक्ति के माता-पिता या उनके माता-पिता ऊपर की डिग्रियों में किसी भी सीमा तक पूर्वज (Ascendant) कहलाते हैं।
(4) साम्पाश्विक (Collaterals)–साम्पार्रिवक बराबर की लाइनों के वंशज होते हैं। वे एक पूर्वज या पूर्वजों के वंशज समान्तर लाइनों में होते हैं। जैसे- भाई-बहन, मामा, मौसी तथा उनकी सन्तान, चाचा, बुआ तथा उनकी सन्तानें, उनकी सन्तान की सन्तान।
(5) गोत्रज (Agnates) – जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी नातेदारी पूर्णतया पुरुष पूर्वजों के माध्यम से अनुरेखण करता है तो वह व्यक्ति गोत्रज कहलाता है। भाई, भाई का पुत्र या पुत्री, चाचा का पुत्र या पुत्री धारा 3 (क) के अनुसार, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक के माध्यम से सम्बन्धित हैं।
(6) बन्धु (Cognates)- जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी नातेदारी किसी स्त्री द्वारा आरेखित करता है तो वह बन्धु (Cognate) कहलाता है। जैसे पुत्री का पुत्र, बहन का पुत्र या पुत्री, नाना, नानी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बन्धु तब कहा जाता है यदि वह रक्त या दत्तक द्वारा दूसरे से सम्बन्धित हो परन्तु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं।
उत्तर– (ii) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने के पश्चात् मिताक्षरा सहदायिक की अवधारणा में काफी सुधार हुआ किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के पारित होने के पश्चात् मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के विभाजन के सम्बन्ध में एक नयी अवधारणा को जन्म दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सहदायिक सम्पत्तियों में पुत्रियों को भी पुत्रों के समान पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो भी असमानतायें सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्त्री और पुरुषों के बीच थीं, वे पूरी तरह से समाप्त कर दी गयीं, जिसकी वजह से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2), धारा 6, धारा 23 व 24 तथा धारा 30 प्रभावित हुई अर्थात् धारा 6 के अन्तर्गत जो व्यवस्था मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में थी, इस संशोधन के द्वारा उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा प्रत्येक स्त्री (पुत्री) को चाहे वह विवाहिता हो अथवा अविवाहिता हो, उसको मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के अन्तर्गत जन्म से अधिकार दे दिया गया और वह सम्पत्ति के विभाजन में पुत्रों के साथ समान भागिता के अन्तर्गत सम्पत्ति को धारण करेगी अर्थात् मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के काल्पनिक विभाजन के सिद्धान्त को इस संशोधन के अन्तर्गत पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और वे सारे अधिकार पुत्रियों को स्वतः अधिरोपित हो गये जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पुत्रों को प्राप्त थे अर्थात् पुत्रों की भाँति पुत्रियों की भी अपनी पैतृक सम्पत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 में भी महत्वपूर्ण संशोधन किये गये जिसके अन्तर्गत जो अधिकार पुत्रों को प्रदत्त थे, वे सभी अधिकार पुत्रियों तथा विधवा स्त्रियों को भी प्रदत्त किये गये अर्थात् वे निवास के साथ-साथ ऐसी सम्पत्ति के बँटवारे की माँग कभी भी उठा सकती हैं और पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति का बँटवारा भी करा सकती हैं तथा पुत्रियाँ अपने पिता के जीवन काल में ही सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकती हैं। धारा 24 को भी इस संशोधन के द्वारा पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इस वर्तमान संशोधन के अन्तर्गत यदि विधवा स्त्री पुनः विवाह कर लेती है तो ऐसी स्थिति में वह अपने पूर्व पति की सम्पत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने से वंचित नहीं होगी। इसके साथ ही पूर्व उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में भी परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के पश्चात् वसीयती उत्तराधिकार के सम्बन्ध में जो व्यवस्था पुत्रों के सम्बन्ध में थी, वे सारी व्यवस्थायें पुत्रियों को भी प्रदत्त की गयीं।
मृतक पुरुष के स्वअर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनुसूची वर्ग-1 में परिवर्तन करते हुए पुत्रियों को भी दो पीढ़ियों को सम्मिलित किया गया जो कि पुत्र एवं पुत्रियों के बीच विभेद को समाप्त करते हैं।
अतः अब हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पुत्र एवं पुत्रियों के बीच के सम्पत्ति विभेद को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।
प्रश्न 24 निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष के उत्तराधिकार से सम्बन्धित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अनुसूची के वर्ग-1 एवं वर्ग-11 में दायादों की सूची क्या है?
Explain the provisions of Hindu Succession Act, 1956 relating to succession of male Hindu dying intestate. What is list of heirs in class-1 and class-11 of the schedule ?
उत्तर – यदि कोई व्यक्ति वसीयत करके मरता है तो आमतौर पर उसकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है जो उसकी वसीयत या इच्छा-पत्र में प्रकट की गई होती हैं। वसीयत या इच्छा पत्र का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसका वसीयतकर्त्ता के जीवनकाल में कोई महत्व नहीं होता क्योंकि वसीयत या इच्छा-पत्र वसीयत करने वाले की मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावी होती है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत में उत्तराधिकारियों को निर्धारित कर दिया है तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाता है। समस्या वहाँ होती है जहाँ कोई निर्वसीयती मर जाता है अर्थात् जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत किये ही मरता है। ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकार को निर्वसीयती उत्तराधिकार कहा जाता है।
धारा 8 से 13 तक के अन्तर्गत हिन्दू पुरुष के निर्वसीयती सम्पत्ति छोड़कर मरने के बाद के उत्तराधिकार का नियम उल्लिखित है। अधिनियम की धारा 8 में उत्तराधिकार के बे सामान्य नियम दिये गये हैं जो किसी पुरुष के द्वारा निर्वसीयती किसी सम्पत्ति को छोड़कर मरने पर लागू होते हैं। यह धारा किसी पुरुष के पृथक् अथवा स्वार्जित सम्पत्ति में न्यागमन की व्याख्या करती है। व्यक्ति को दाय में प्राप्त सम्पत्ति भी उसकी निजी अथवा पृथक् सम्पत्ति मानी जाती है और उसके सम्बन्ध में उसके अपने पुत्रों को कोई जन्मतः अधिकार नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वह संयुक्त सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती। इस धारा में दायादों की सम्पत्ति को उत्तराधिकार के उद्देश्य से चार वर्गों में विभाजित किया गया है –
(1) अनुसूची के वर्ग में उल्लिखित नातेदार
(2) अनुसूची के वर्ग 2 में उल्लिखित नातेदार;
(3) मृतक के सपित्र्य (गोत्रज) (Agnates);
(4) मृतक के साम्पाश्विक (बन्धु) (Cognates) |
अधिनियम के अन्तर्गत इन दायादों द्वारा उत्तराधिकार में सम्पत्ति न प्राप्त कर सकने पर मृतक को सम्पत्ति सरकार को न्यागत हो जाती है, जिसको सम्पत्ति का राजगामी होना कहा जाता है। राज्य को दायादों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अतः सरकार (राज्य) को पाँचवें वर्ग के दायादों की कोटि में रखकर एक वर्ग अलग से नहीं बना दिया गया और इसी कारण से दायादों के केवल चार ही वर्गों का अधिनियम में वर्णन किया गया है धारा 8 स्पष्ट हो जाता है –
निर्वसीयती मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी –
(क) प्रथमतः उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं,
(ख) द्वितीयतः यदि वर्ग 2 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं,
(ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रज को तथा
(घ) अन्ततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को।
इस आरेख में सभी नातेदार अनुसूची के वर्ग में उल्लिखित हैं। अतः वे वर्ग 2 में उल्लिखित दायादों के अपवर्जन में ‘क’ की छोड़ी गई सम्पत्ति में ‘क’ की मृत्यु के बाद दाय प्राप्त करेंगे। इस आरेख में ‘त’, ‘थ’ तथा ‘द’, ‘क’ के पूर्व मृत पुत्र की सन्तान हैं। इसी प्रकार ‘य’, ‘र’ तथा ‘ल’ पूर्व मृत पुत्री की सन्तान हैं। अतः वे भी वर्ग 1 के उत्तराधिकारी हैं और वे अपने पिता और माता के अंश का संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे।
रामाबाई पद्माकर बनाम रुक्मणिबाई विष्णु विखण्ड, ए० आई० आर० 2003 एस० सी० 3109 के बाद में एक हिन्दू पुरुष अपनी सम्पत्ति 7 पुत्रियों एवं विधवा पत्नी के बीच छोड़कर मरता है। पति की मृत्यु के समय पुत्रियाँ वयस्क थीं। सम्पूर्ण सम्पत्ति उसकी पत्नी के संरक्षण में थी। पुत्रियों की माँ ने ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त किया था, एक विधवा पुत्री के पक्ष में वसीयत के माध्यम हस्तान्तरित कर दिया था। अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा वाद लाने पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधवा माँ जो सम्पत्ति अपने पति के मृत्योपरान्त प्राप्त की थी, उस सम्पत्ति में उसके अलावा उसकी सात पुत्रियों का भी बराबर से हिस्सा लगेगा अर्थात् प्रत्येक को 1/8 भाग प्राप्त होगा। न्यायालय ने इस वाद में विधवा द्वारा प्रतिपादित की गयी वसीयत की वैधता को भी उचित ठहराया और यह अभिनिर्धारित किया कि वह पुत्री जिसके पक्ष में वह वसीयत की गयी थी, अपनी माँ के 1/8 भाग को हिस्से में प्राप्त करेगी अर्थात् वह पुत्री 1/8 भाग अपनी माँ की वसीयत के माध्यम से तथा 1/8 भाग विभाजन के माध्यम से ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त करेगी।
भँवर सिंह बनाम पूरन व अन्य, ए० आई० आर० (2008) एस० सी० 1490 के बाद में एक हिन्दू पुरुष अपनी सम्पत्ति में एक पुत्र एवं तीन पुत्रियों के बीच छोड़कर मरता है तथा मृत्यु के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारियों ने ऐसी सम्पत्ति में धारा 8 के अधीन आपस में 1/4 भाग का अंश प्राप्त कर लिया था। प्रस्तुत वाद में वादी के पिता ने संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति को बिना किसी जरूरत के ही विक्रय कर दिया था। न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत किया गया कि वादी के पिता द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति का विक्रय अवैध था, वह केवल अपने हिस्से की सम्पत्ति का ही विक्रय कर सकता है, जो सम्पत्ति उसने बँटवारे के परिणामस्वरूप अपने हिस्से में प्राप्त किया था।
श्रीमती पट्टनारानी कर्माकर बनाम भोला नाथ चन्द्रा, ए० आई० आर (2013) कलकता (NOC) 166 के मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ कोई हिन्दु पुरुष निर्वसौयती सम्पत्ति को छोड़कर मरता है और उसके मृत्युपरान्त उसके पुत्र एवं पुत्रियों मौजूद हाँ वहाँ उसके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति का न्यागमन उसके पुत्र एवं पुत्रियों के बोध होगा अर्थात् उसके पुत्र एवं उसकी पुत्रियों को ऐसी सम्पत्ति में बराबर से हिस्सा प्राप्त होगा। अभी हाल में पुन: उच्चतम न्यायालय ने रोहित चौहान बनाम सुरेन्द्र सिंह, ए० आई० आर० (2013) एस० सी० 3525 के मामले में यह निर्णीत किया कि जब किसी सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन हो चुका है तो विभाजन के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति स्व-अर्जित सम्पत्ति के रूप में मानी जायेगी और उस सम्पत्ति का विभाजन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत होगा। उपरोक्त मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसी सहदायिक सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात् उसके परिवार में किसी पुत्र अथवा पुत्री का जन्म हुआ हो तो ऐसी सम्पत्ति में पुत्र अथवा पुत्रों का जन्मतः कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।
श्रीमती नारायणी बाई बनाम हरियाणा राज्य, ए० आई० आर० 104) पंजाब एवं हरियाणा राज्य (2006) के बाद में कहा गया कि अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, कोई विवाहिता पुत्री भी अपने मृतक पिता जिसकी निर्वसीयत में मृत्यु हो गई, की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होने का हक रखने वाली प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है।
धारा 9 के अनुसार, अनुसूची के प्रथम वर्ग के दायाद एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। द्वितीय वर्ग के दायाद तब तक अपवर्जित किये जाते हैं जब तक प्रथम वर्ग का कोई भी दायाद प्राप्त होता है। “वर्ग (1) के दायाद एक साथ और अन्य सब दायादों को अपवर्जित करके अंशभागी होंगे। वर्ग (2) में प्रथम प्रविष्टि में के दायाद दूसरी प्रविष्टि में के दायादों को अपेक्षा अधिमान्य होंगे। द्वितीय प्रविष्टि में के दायादों को तृतीय प्रविष्टि में के दायादों की अपेक्षा अधिमान्यता प्राप्त होगी और इसी प्रकार से अन्य प्रविष्टि के लोग क्रम से अधिमान्य होंगे।”
वर्ग (1) में उल्लिखित दायादों की सूची– वर्ग (1) में उल्लिखित मृतक के दायादों की सूची इस प्रकार है –
(1) पुत्रः
(2) पुत्री;
(3) विधवा पत्नी;
(4) माता;
(5) पूर्व मृत पुत्र का पुत्र;
(6) पूर्व मृत पुत्र की पुत्री;
( 7 ) पूर्व मृत पुत्री का पुत्र;
(8) पूर्व मृत पुत्री की पुत्री;
(9) पूर्व मृत पुत्री की विधवा पत्नी;
(10) पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र;
(11) पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री तथा
(12) पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा पत्नी।
जैसे- एक हिन्दू पुरुष एक विधवा पत्नी तथा पिता को छोड़कर निर्वसीयत मर जाता है, तो विधवा पत्नी पिता को अपवर्जित करके समस्त सम्पत्ति की दायाद होगी।
धारा 10 के अनुसार निर्वसीयती की सम्पत्ति उसके दायादों में जो अनुसूची के वर्ग (1) में दिये गये हैं, निम्न नियमों के अनुसार विभाजित (वितरित) की जायेगी –
नियम 1- निर्वसीयत के विधवा या यदि एक से अधिक विधवा हो तो सब विधवायें मिलकर एक अंश लेंगी। नियम 2- निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियाँ और माता प्रत्येक एक-एक अंश प्राप्त करेंगी।
नियम 3- निर्वसीयत के पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्रियों में से प्रत्येक को शाखा में आने वाले दायाद मिलकर एक अंश लेंगे।
नियम 4 – नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण (i) पूर्व मृत पुत्र की शाखा में वर्तमान दायादों के बीच इस प्रकार किया जायेगा कि उसकी अपनी विधवा या विधवाओं को (मिलाकर) और उत्तरजीवी पुत्र, पुत्रियों को समान प्रभाग प्राप्त हो; और उनके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वैसा ही प्रभाग प्राप्त हो ।
(ii) पूर्व मृत पुत्री की शाखा में आने वाले दायादों में वितरण इस प्रकार किया जायेगा कि उत्तरजीवी पुत्र एवं पुत्रियों को समान प्रभाग प्राप्त हो।
नियम 5– इस नियम के अनुसार निर्वसीयत की विधवा पत्नी एक अंश की हकदार है। जहाँ निर्वसीयत एक से अधिक विधवाओं को छोड़कर मरा है, वहाँ सभी विधवायें एक साथ एक अंश को हकदार होंगी तथा यह अंश पुत्र अथवा पुत्री के अंश के बराबर होगा।
‘अ’ एक माता, दो विधवायें, तीन पुत्रों तथा तीन पुत्रियों को छोड़कर मरता है। दो विधवायें एक साथ मिलकर एक अंश ग्रहण करेंगी। इस प्रकार कुल मिलाकर आठ अंश होंगे। प्रत्येक पुत्री, माता एवं दोनों विधवायें मिलकर सम्पत्ति का 1/8 अंश प्राप्त करेंगी।
वर्तमान अधिनियम में दत्तक पुत्र तथा बाद में उत्पन्न हुए औरस पुत्र में कोई भेद नहीं किया गया है। उनमें से प्रत्येक एक अंश का हकदार है। पूर्व हिन्दू विधि का यह नियम कि दत्तक पुत्र बाद में उत्पन्न हुए औरस पुत्र से कम अंश में दाय ग्रहण करेगा, अब अधिनियम की धारा 4 के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है।
उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 (ब) के अनुसार, अनुसूची के वर्ग 2 में उल्लिखित दायाद तभी उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे जबकि वर्ग में के दायाद नहीं रह गये हैं। धारा 11 जो इस प्रकार वर्ग 2 के दायादों में सम्पत्ति के वितरण को संनियन्त्रित करती है, इस प्रकार है –
“निर्वसीयती की सम्पत्ति अनुसूची के वर्ग 2 में की किसी एक प्रविष्टि में उल्लिखित दायादों के बीच इस प्रकार विभाजित की जायेगी कि उन्हें समान अंश प्राप्त हो।”
इस प्रकार जहाँ प्रविष्टि का केवल एक ही दायाद है, वहाँ वही समस्त सम्पदा का अधिकारी होगा अथवा होगी, किन्तु जब एक से अधिक अधिमान्य दायाद उस प्रविष्टि में हैं तो उस अवस्था में इस प्रकार के सभी दायाद बराबर-बराबर अंश ग्रहण करेंगे तथा निर्वसीयती के सगे सम्बन्धी चचेरे सम्बन्धी की अपेक्षा अधिमान्य होंगे।
अनुसूची के वर्ग 2 में उल्लिखित दायादों की सूची –
(1) पिता
(2) (क) पुत्र की पुत्री का पुत्र
(ख) पुत्र की पुत्री की पुत्री
(ग) भाई।
(घ) बहन।
(3) (क) पुत्री के पुत्र का पुत्री।
(ख) पुत्री के पुत्र की पुत्री
(ग) पुत्री की पुत्री का पुत्र।
(घ) पुत्री की पुत्री की पुत्री ।
(4) (क) भाई का पुत्र।
(ख) बहन का पुत्र
(ग) भाई की पुत्री
(घ) बहन की पुत्री।
(5) (क) पिता का पिता; तथा
(ख) पिता की माता।
(6) (क) पिता की विधवा
(ख) भाई की विधवा पत्नी।
(7) (क) पिता का भाई; तथा
(ख) पिता की बहन।
(8) (क) माता का पिता।
(ख) माता की माता।
(9) (क) माता का भाई।
(ख) माता की बहन
के० राज बनाम मुथ्थम्मा, ए० आई० आर० (2001) एस० सी० 1720 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 2 के अन्तर्गत यह निर्णय दिया कि अनुसूची 2 में बहन शब्द के अन्तर्गत सहोदर बहन अपने पितृपक्ष की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई दावा अन्य पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकती, अर्थात् जहाँ एक ही माता हो लेकिन सन्तान कई पिता से उत्पन्न हुई हों ऐसी स्थिति में सहोदर बहनों को अन्य पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।
प्रश्न 25. हिन्दू स्त्री के निर्वसीयत सम्पत्ति के उत्तराधिकार से सम्बन्धित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
Explain the provisions of Hindu Succession Act, 1956 regarding succession to the Property of a female Hindu dying intestate.
उत्तर– स्त्री की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में नियम (Rule of Succession to the Property of Females)– एक हिन्दू महिला (स्त्री) सहदायिक (Coparcener) नहीं मानी जाती थी। अतः पुरानी मिताक्षरा विधि के अनुसार संयुक्त हिन्दू सम्पत्ति में स्त्री सदस्य को कोई हित प्राप्त नहीं है। एक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में स्त्री सदस्य को विभाजन को माँग करने का अधिकार नहीं है। पुरानी हिन्दू विधि के अन्तर्गत स्त्री सिर्फ भरण-पोषण की माँग कर सकती है। परन्तु नवीन हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के द्वारा हिन्दू महिला को संयुक्त सम्पत्ति में पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है तथा इस अधिकार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में मान्यता दी गई है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 एक निर्वसीयती हिन्दू के मरने पर उसके उत्तराधिकार के दो नियम प्रतिपादित करती है। यदि निर्वसीयती के मरने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रथम श्रेणी के सिर्फ पुरुष वारिस ही हैं तो सम्पत्ति का न्यागमन पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार उत्तरजीविता के नियमों के अनुसार होगा परन्तु यदि प्रथम श्रेणी के वारिसों में महिला वारिस भी है तो सम्पत्ति का न्यागमन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से 12 तक के प्रावधानों के अनुसार होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, महिला वारिस, पुरुष वारिसों के समान अनुपात में अंश ग्रहण करते हैं।
पर अब हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, धारा 6 में जो व्यवस्था मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में थी, इस संशोधन के पश्चात् उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब प्रत्येक स्त्री (पुत्री) को चाहे वह विवाहिता हो अथवा अविवाहित हो, उसका मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के अन्तर्गत जन्म से अधिकार दे दिया गया और वह सम्पत्ति के विभाजन में पुत्रों के साथ समान भागिता के अन्तर्गत सम्पत्ति को धारण करेगो अर्थात् मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति के काल्पनिक विभाजन के सिद्धान्त को इस संशोधन के अन्तर्गत पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और वे सारे अधिकार पुत्रियों को स्वतः अधिरोपित हो गये जो पुत्रों को प्राप्त थे अर्थात् पुत्रों की भाँति पुत्रियों की भी अपनी पैतृक सम्पत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी।
हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 ने स्त्री की सम्पत्ति सम्बन्धी परिकल्पना में आमूल परिवर्तन किया है। धारा 14 के अनुसार स्त्री उसे प्राप्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी है। अब सम्पत्ति के हस्तान्तरण के स्त्री के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु यदि स्त्री निर्वसीयत मरती है तो उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए स्त्री को सम्पत्ति का सोत अब भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्त्री की सम्पत्ति को उसके स्रोत के आधार पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है
(1) पिता या माता से प्राप्त सम्पत्ति
(2) उसके पति या ससुर से प्राप्त सम्पत्ति
(3) अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति उपरोक्त स्रोतों का महत्व स्त्री के सन्तानहीन मरने पर है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 एक ऐसी स्त्री के सम्बन्ध में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का प्रतिपादन करती है जो निर्वसीयती (Intestate) मरती है क्योंकि यदि कोई महिला वसीयत करके मरती है तो उसके उत्तराधिकार के निर्धारण में उसकी इच्छाओं का सम्मान होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 16, धारा 15 में विहित विभिन्न श्रेणी के वारिसों (Various categories of heirs) में उत्तराधिकार के कम का निर्धारण करती है। धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्त्री के उत्तराधिकार पाँच प्रविष्टियों में बाँटे गये हैं। पाँचों प्रविष्टियों में उत्तराधिकारियों के न होने पर सम्पत्ति सरकार को जाती है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 निम्न है –
धारा 15- एक हिन्दू स्त्री जो निर्वसीयती मरती है, उसकी सम्पत्ति इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निम्न पर न्यागमित होगी –
(1) प्रथमतः पुत्रों तथा पुत्रियों पर (जिसमें किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्रों की सन्ताने सम्मिलित हैं) तथा उसके पति पर। ‘क’ एक महिला अपने पीछे पुत्र तथा पुत्री तथा पति को छोड़कर निर्वसीयत भरती है तो उसकी सम्पत्ति उसके पुत्र तथा पुत्री तथा उसके पति को प्राप्त होगी।
(2) द्वितीयतः उसके पति के वारिसों पर अर्थात् यदि उसके पुत्र, पुत्री या पति नहीं हैं तो उसकी सम्पत्ति उसके पति के वारिसों पर न्यागमित (devolve) होगी।
(3) तृतीयत: उसकी माता तथा पिता पर यदि मृतक महिला के पुत्र, पुत्री, पति या पति के वारिस नहीं हैं तो उसकी सम्पत्ति उसकी माता तथा पिता को प्राप्त होगी।
(4) चतुर्थतः यदि निर्वसीयती मृतक स्त्री के पुत्र, पुत्री, पति पति के वारिस या माता-पिता नहीं हैं तो उसकी सम्पत्ति उसके पिता के वारिसों को प्राप्त होगी।
(5) अन्त में यदि उसके पुत्र, पुत्री, पति के वारिस, माता-पिता या पिता के वारिस नहीं हैं तो उसकी सम्पत्ति उसको माता के वारिसों को प्राप्त होगी।
धारा 15 की उपधारा (2), उपधारा (1) के विस्तार को सीमित करती है तथा यह उपधारा (1) की परन्तुक है। धारा 15 की उपधारा (2) (क) के अनुसार यदि किसी हिन्दू स्त्री को सम्पत्ति उसके माता-पिता से प्राप्त है और उसके पुत्र या पुत्री (जिसमें मृत पुत्र या पुत्री की सन्तान सम्मिलित है) नहीं हैं तो उसके माता पिता से प्राप्त सम्पत्ति धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित वारिसों में न्यागमित न होकर उसके पिता के वारिसों को प्राप्त होगी न्यागमित होगी।
धारा 15 की उपधारा (2) (ख) के अनुसार, यदि किसी महिला ने सम्पत्ति अपने पति या ससुर (Husband or Father-in-law) से उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा उसके पुत्र या पुत्री या पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की सन्तान नहीं है तो उसकी सम्पत्ति उपधारा (1) में उल्लिखित उसके वारिसों को प्राप्त न होकर उसके पति के वारिसों में न्यागमित होगी।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15. उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो स्त्री इस अधिनियम की धारा 14 उपधारा (2) के अर्थों में सीमित परिसम्पत्ति (Limited Estate) के रूप में धारण करती है। धारा 15 के नियम किसी स्त्री की उस सम्पत्ति के सन्दर्भ में ही लागू होते हैं, जो वह स्त्री पूर्ण स्वामी (absolute owner) के रूप में धारण करती हो।
मुसम्मात मोकुन्देरो बनाम करतार सिंह, ए० आई० आर० 1991 एस० सौ. 257 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जहाँ एक स्त्री सीमित स्वामी (Limited owner) के रूप में सम्पत्ति धारण करती है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन (लागू) होने के पश्चात् वह उस सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी बन जाती है, ऐसी सम्पत्ति के न्यागमन (devolution) के सम्बन्ध में धारा 15 तथा धारा 16 के प्रावधान लागू होंगे। उदाहरण के लिए एक स्त्री अपने पीछे अपने पूर्व मृत पुत्र की पुत्री तथा अपनी ननद (पति की बहन) को छोड़कर निर्वसीयत मरती है तो धारा 15 तथा 16 के अन्तर्गत उसके पूर्व मृत पुत्र की पुत्री उसको सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी। उसकी ननद को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पूर्व मृत पुत्र की पुत्री धारा 15 (क) में उल्लिखित बारिस (Heir) है तथा वह अन्य वारिसों को अपवर्जित करेगी।
धारा 15 (1) में सन्दर्भित पुत्र तथा पुत्री में निर्वसीयत मरने वाली स्त्री के सभी पुत्र या पुत्री सम्मिलित हैं चाहे वे उसके पूर्व पति से उत्पन हुए हों या पश्चात् से पुत्र या पुत्री में अवैध पुत्र (Illegitimate son) भी सम्मिलित है। परन्तु इसमें सौतेला पुत्र सम्मिलित नहीं है। सौतेले पुत्र से तात्पर्य उसके पति की पूर्व पत्नी से उत्पन्न पुत्र से है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, चूँकि मिताक्षरा विधि रक्त सम्बन्ध की निकटता को मान्यता देती है। अतः उस महिला के गर्भ से उत्पन्न पुत्री उसकी सम्पत्ति प्राप्त करेंगे चाहे वे पूर्व पति या पश्चात् (दूसरे) पति से उत्पन्न हुए हों। परन्तु उसके पति से अन्य महिला को उत्पन्न पुत्र या पुत्री सम्मिलित नहीं हैं। [लक्ष्मण सिंह बनाम किरपा सिंह, ए० आई० आर० 1987 एस० सी० 1616]
पुत्र शब्द में प्राकृतिक (natural) तथा दत्तक (adopted) पुत्र भी सम्मिलित हैं। इसमें ऐसे पुत्र भी सम्मिलित हैं जो उसके पुनर्विवाह के पश्चात् उत्पन्न हुए हों। इसमें महिला के अवैध पुत्र (Illegitimate son) भी सम्मिलित हैं।
‘क’ अपनी विधवा तथा दो पुत्रों को छोड़कर मरता है। इन दो पुत्रों से एक उसकी पूर्व पत्नी से तथा एक उसकी वर्तमान विधवा पत्नी से उत्पन्न है। यदि विधवा निर्वसीयत मरती है तो उसकी सम्पत्ति उसके पति की पूर्व पत्नी से उत्पन्न पुत्र को नहीं प्राप्त होगी, उसकी सम्पत्ति विधवा से उत्पन्न पुत्र को प्राप्त होगी। [आनन्द राव बनाम गोविन्द राव झिंगराणी, ए० आई० आर० 1984 बाम्बे 338]
बी० हथराज बनाम एम० श्री देवी, ए० आई० आर० (2014) कर्नाटक 58 के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि जहाँ किसी स्त्री को अपने माता-पिता से सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और वह निःसन्तान हो वहाँ ऐसी सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके माता-पिता के दायादों में वापस चली जायेगी न कि उसके पति के दायादों में न्यागत होगी।
एक विधवा ‘क’ अपने दूसरे पति से सम्पत्ति प्राप्त करती है। उसका एक पुत्र ‘च’ उसके पूर्व पति से उत्पन्न है न कि दूसरे पति से महिला की मृत्यु के पश्चात् उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को सम्पत्ति प्राप्त होगी भले ही उसने सम्पत्ति पश्चात्वर्ती पति से उत्तराधिकार में
प्राप्त की है क्योंकि धारा 15 उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र का वारिस मानती है भले ही वह पुत्र
पति से उत्पन्न हुआ हो या पश्चात्वर्ती पति से जिससे उसने सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की
थी। [ रोशन लाल बनाम दलीप, ए० आई० आर० 1985 हिमाचल प्रदेश 8]
एक हिन्दू स्त्री अपने पिता द्वारा दान में प्राप्त सम्पत्ति की आज्ञप्ति के फलस्वरूप एक सम्पत्ति प्राप्त करती है। वह अपने पीछे भाई तथा पति को छोड़कर मरती है। धारा 15 (2) के अन्तर्गत निर्धारित नियम के अनुसार यह सम्पत्ति उसके भाई को प्राप्त होगी न कि उसके पति को क्योंकि सम्पत्ति उसके पिता से प्राप्त है। [ चेट्टीयार बनाम चेट्टीयार, ए० आई० आर० 1976 मद्रास 154. रघुवीर बनाम जानकी प्रसाद, ए० आई० आर० 1981 एम० पी० 39]
उत्तराधिकार का क्रम तथा सम्पत्ति का वितरण (Order of Succession and distribution )-धारा 15 (1) में निर्धारित वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम तथा उनके मध्य सम्पत्ति के वितरण के बारे में नियम इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है।
इस धारा में इस सम्बन्ध में तीन नियम निर्धारित किये गये हैं
( 1 ) नियम 1- इस नियम के अनुसार इस अधिनियम की धारा 15 (1) में दी गई प्रविष्टियों (Entries) में प्रथम प्रविष्टि (First Entry) के वारिस सम्पत्ति में एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक उत्तराधिकारी समान रूप से एक भाग प्राप्त करेगा। प्रथम प्रविष्टि के वारिस द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करेंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्रविष्टि के उत्तराधिकारी तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम् प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को तथा चतुर्थ प्रविष्ट के उत्तराधिकारी पंचम प्रविष्टि के उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करेंगे।
प्रथम प्रविष्टि पुत्र, पुत्री तथा पति
द्वितीय प्रविष्टि पति के वारिस
तृतीय प्रविष्टि माता-पिता
चतुर्थ प्रविष्टि पिता के वारिस
पंचम् प्रविष्टि माता के वारिस
नियम 2- यदि निर्वसीयती स्त्री के पुत्र या पुत्री उसके मरने के पूर्व मर गये हैं तथा निर्वसीयती स्त्री के मरने के समय उनकी सन्ताने जीवित हैं तो पूर्व मृत पुत्र या पुत्रियों के पुत्र या पुत्रियाँ उसी अनुपात में निर्वसीयती स्त्री की सम्पत्ति ग्रहण करेंगे जिस अनुपात में उनकी माता-पिता प्राप्त करते यदि वे जीवित होते।
नियम 3- धारा 16 को उपधारा (2) में तथा उपधारा (1) के खण्ड (S) तथा (क) एवम् (ङ) में उल्लिखित वारिसों पर निर्वसीयती स्त्री की सम्पत्ति का न्यागमन (deyolution) उसी क्रम में तथा उन्हीं नियमों के अनुसार होगा जो तब लागू होते यदि सम्पत्ति पिता की या माता की या पति की होती तथा ऐसी माता या पिता या पति निर्वसीयती स्त्री की मृत्यु तत्काल पश्चात् निर्वसीयती मरा होता
धारा 15 तथा धारा 16 का अध्ययन इस सन्दर्भ में एक साथ करना उपयुक्त (appropriate) होगा। धारा 15 की उपधारा (1) निर्वसीयती स्त्री के वारिसों को पाँच श्रेणियों में विभक्त करती है। वारिसों का विशिष्टीकरण नहीं किया गया है। उनका वर्गीकरण मृतक के पति, माता तथा पिता से उनके सम्बन्धों के कारण किया गया है। स्त्री को प्राप्त स्त्रीधन भी इस धारा के अन्तर्गत स्त्री की सम्पत्ति मानी जायेगी तथा धारा 15 तथा धारा 16 में निर्धारित नियम स्त्री के स्त्रीधन पर भी लागू होगा।
बसन्ती देवी रवि प्रकाश बनाम राम प्रसाद जायसवाल, ए० आई० आर० (2008) एस० सी० 295 के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ कोई हिन्दू स्त्री अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को निर्वसीयत छोड़कर मर जाती है और उसके परिवार में उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसी सम्पत्ति का न्यागमन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत गोत्रज को प्राप्त होगा।
प्रश्न 26. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्तराधिकार की अनर्हता (Disqualifications) का संक्षेप में उल्लेख करें।
What are the disqualifications for the heir to inherit the property under Hindu Succession Act, 1956?
उत्तर– पुरानी हिन्दू विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कई निरर्हताओं को मान्यता प्राप्त थी। यदि कोई व्यक्ति किसी निरर्ह व्यक्ति के माध्यम से उत्तराधिकार का अधिकार रखता था तो वह भी उस व्यक्ति की निरर्हता के कारण उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाता था। परन्तु यदि निरहित उत्तराधिका उत्तराधिकार के आरम्भ होने से पूर्व अपनी निरर्हता से मुक्त हो जाता था तो वह उत्तराधिकार में अपना भाग प्राप्त कर सकता था क्योंकि निरर्ह उत्तराधिकारी के बारे में यह उपधारणा होती थी कि वह उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न होने से पूर्व मर चुका है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 27 इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान करती है –
“यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को उत्तराधिकार (विरासत) में पाने से अधिनियम के अन्तर्गत निरर्हित (disqualified) या अयोग्य हो तो वह सम्पत्ति ऐसे न्यागत (devolve) होगी जैसे कि ऐसा व्यक्ति निर्वसीयत (Intestate) के पूर्व मर चुका हो।”
‘अ’, अपनी विधवा ‘क’ तथा विधवा पुत्रवधू ‘ख’ को छोड़कर 1974 में मरा ‘ख’ पुत्रवधू ने 1973 में पुनर्विवाह कर लिया। पुनर्विवाह एक निरर्हता है। अत: ‘ख’ 1973 में उत्तराधिकार से निरर्ह हो गई। अब ‘अ’ की विधवा ‘क’ ‘अ’ की सम्पत्ति उत्तराधिकार में वैसे ही प्राप्त करेगी जैसे ‘ख’ ‘अ’ की 1974 में मृत्यु होने से पूर्व 1973 में मर चुकी थी।
‘क’ अपने भाई ‘च’, भतीजे ‘छ’ तथा दादी ‘प’ को छोड़कर मरता है। भाई ‘च’ उत्तराधिकार के लिए निरर्ह है। अतः भतीजा ‘छ’ उत्तराधिकार के लिए निरर्ह होगा और यह उपधारणा होगी कि ‘छ’, ‘क’ के पूर्व मर चुका है। अत: ‘क’ की सम्पत्ति उसकी दादी को न्यागमित होगी।
पुरानी हिन्दू विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकार से सम्बन्धित कई निरर्हतायें थीं। नवीन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने इन निरर्हताओं को काफी कम कर दिया है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निम्न निरर्हताएं है –
(1) रोग या अंग विकार (Disease or deformity) (धारा 28 ) – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी निरर्हता को छोड़कर किसी अन्य कारण उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं होगा चाहे वह निरर्हता रोग या अंग विकार (disease or deformity) ही क्यों न हो अर्थात् यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी रोग या अंगविकार (अंधेपन, बहरेपन या अन्य अंग विकार) के आधार पर उत्तराधिकार से वंचित नहीं होगा।
(2) शीलभ्रष्टता (Inchastity)- शीलभ्रष्टता या व्यभिचार भी उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्तराधिकार के लिए निरर्हता (Disqualification) नहीं है। अतः एक शीलभ्रष्ट महिला (स्त्री) उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं की जा सकेगी। [चाँदी बनाम गजाधार, ए० आई० आर० 1976 कलकत्ता 356]
(3) पुनर्विवाह (Remarriage)– किसी व्यक्ति की पत्नी को उसकी मृत्यु के पश्चात् पुनर्विवाह करने के आधार पर अपने पति की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 विधवा के पुनर्विवाह को उत्तराधिकार के लिए निरर्हता नहीं मानता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 24 [ धारा 24 हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा विलोपित कर दिया गया है] के अनुसार मृत व्यक्ति का विधवा के पुनर्विवाह का प्रश्न उत्तराधिकार खुलने के के समय नहीं उठ सकता। मृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पुनर्विवाह करने पर स्त्री उत्तराधिकार प्राप्त सम्पत्ति को पाने के लिए निरहित नहीं की जा सकती परन्तु उत्तराधिकार खुलने से पूर्व यदि विधवा पुत्रवधू, विधवा पौत्र वधू अथवा विधवा भाभी ने पुनर्विवाह कर लिया है तो वे त व्यक्ति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार पाने के लिए निरर्ह (disqualified : अयोग्य) हो। जायेंगी। संशोधन अधिनियम, 2005 से पुनर्विवाह सम्बन्धी निर्योग्यता समाप्त कर दी गयी तथा पुत्र की विधवा, पौत्र की विधवा, भाई की विधवा यदि पुनः विवाहिता है तो भी वह उत्तराधिकार पाने की हकदार होगी। विधवा माता या विधवा सौतेली माता या विधुर पिता के लिए पुनर्विवाह (Disqualification) या अयोग्यता नहीं है। [श्रीमती कस्तूरी देवी बनाम उपनिदेशक चकबन्दी, ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 2295]
(4) संपरिवर्तन या धर्म परिवर्तन (Conversion)- किसी उत्तराधिकारी का धर्म परिवर्तन उसके उत्तराधिकार के अधिकार के लिए निरर्हता (Disqualification) या अयोग्यता नहीं है परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अनुसार धर्म परिवर्तित या सम्परिवर्तित व्यक्ति के वंशज उत्तराधिकार के लिए निरर्ह (disqualified) हो जाते हैं। सम्परिवर्तित व्यक्ति के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं। प्राचीन हिन्दू विधि में सम्परिवर्तित व्यक्ति या धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में उत्तराधिकार के लिए निरर्ह (disqualified) हो जाता था परन्तु जाति निरर्हता निराकरण अधिनियम, 1850 द्वारा इस निरर्हता का निराकरण कर दिया गया है। अब स्थिति यह है कि सम्परिवर्तित व्यक्ति तो उत्तराधिकारी है परन्तु उसकी सन्तान नहीं। परन्तु यदि उसकी सन्तान उत्तराधिकार के समय सम्परिवर्तित न होकर हिन्दू बनी रहती है तो वह उत्तराधिकार से निरर्ह नहीं होगी। इस अधिनियम की धारा 26 पूर्वगामी प्रभाव (Retrospective effect) वाली है तथा उन व्यक्तियों पर भी प्रभावित होगी जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व सम्परिवर्तित हुए थे।
इसे उदाहरण से समझें –
‘अ’ के तीन पुत्र हैं—’क’, ‘ख’ तथा ‘ग’। ‘ग’, ‘अ’ के जीवन काल में मुसलमान हो जाता है। ‘अ’ की मृत्यु पर ‘ग’ अपने भाइयों ‘क’ तथा ‘ख’ के साथ ‘अ’ की सम्पत्ति में 1/3 भाग उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। परन्तु यदि ‘ग’, ‘अ’ के जीवन काल में सम्परिवर्तन (Conversion) के पश्चात् दो पुत्र ‘च’ तथा ‘छ’ को छोड़कर मरता है तो ‘च’ और ‘छ’ को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। परन्तु यदि ‘प’; ‘ग’ का पुत्र उसके सम्परिवर्तन से पूर्व उत्पन्न हुआ है तो वह हिन्दू ही रहा है। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो ‘प’ ‘अ’ की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करेगा।
(5) हत्यारा (Murderer) – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जिससे उसे उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करनी है या उसकी हत्या को दुष्प्रेरित किया है तो वह मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है।
धारा 25 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने स्वयं हत्या की है या हत्या को दुष्प्रेरित किया है वह हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकता। वह ऐसी सम्पत्ति में उत्तराधिकार पाने के लिए निरर्हता प्राप्त कर लेगा जिसके उत्तराधिकार को अग्रसारित (Further) करने के प्रयोजन से उसने हत्या की है या हत्या को दुष्प्रेरित (Abet) किया है। हत्या के आधार पर अधिरोपित निरर्हता प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में लागू होती है जिसको उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति तब अर्ह या योग्य होता है यदि उसने हत्या न की होती या हत्या का दुष्प्रेरण न किया होता। चूँकि निरर्हता प्राप्त व्यक्ति की सम्पत्ति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती, उस पर न्यागमित नहीं होती अतः उसकी सन्तानें या उसके (हत्यारे) के उत्तराधिकारी भी उत्तराधिकार से वंचित हो जाते हैं।
एन० सीतारमैय्या बनाम रामकृष्णैया, ए० आई० आर०1970 आन्ध्र प्रदेश 407 नामक वाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ अपने पिता पर घातक हमले में भाग लिया है तथा अन्य व्यक्तियों को सजा हो गई है परन्तु उसे सन्देह का लाभ देकर धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया गया है या दण्ड कम कर दिया गया है तो भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 तथा 27 उस पर लागू होगी तथा उसे अपने मृत पिता के किसी भी हित में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा।
चमन लाल बनाम मोहन लाल, ए० आई० आर० 1977 दिल्ली 97 नामक बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि जहाँ एक विधवा पर उसके पति की हत्या के लिए विचारण हुआ है तथा अन्त में उसे आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था, उसे अपने मृत पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।
हत्या के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध (Culpable homicide) तथा अवैध हत्या (Unlawful manslaughter) भी आते हैं। [वेंकट बनाम गिरिमायप्पा, (1924) 61 इण्डियन अपील 368]
धारा 25 तथा धारा 27 के अन्तर्गत हत्या के आधार पर निरर्हता के लिए यह आवश्यक है कि हत्या उत्तराधिकार को अग्रसारित करने के लिए की गई है। उदाहरण के लिए ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ का पिता है। ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ के मध्य झगड़े में बीच-बचाव करते समय ‘ख’ उस पर घातक हमला कर देता है, ‘क’ मर जाता है। ‘ख’ हत्या के आधार पर निरर्हता प्राप्त नहीं करेगा तथा उत्तराधिकार से वंचित नहीं होगा।
प्रश्न 27. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित किये गये उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की विवेचना कीजिये।
Explain general rule of succession mentioned under the Hindu Succession Act, 1956.
उत्तर– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 18 से 28 तक उत्तराधिकार के सामान्य नियमों (General rules of Succession) की चर्चा की गई है। ये नियम सभी प्रकार के निर्वसीयती उत्तराधिकार पर लागू होते हैं चाहे सम्पत्ति निर्वसीयती पुरुष या निर्वसीयती स्त्री द्वारा छोड़ी गई है। ये नियम इस अधिनियम की धारा 5 से 17 तक निर्धारित उत्तराधिकार के विशिष्ट नियमों के सम्पूरक (Supplementary) हैं। ये नियम सिर्फ स्पष्टीकरण मात्र ही नहीं हैं। इनमें से कुछ उत्तराधिकार के सारवान् नियमों (Substantive rules of Succession) को प्रतिपादित करते हैं। ये नियम निम्न हैं –
(1) पूर्ण रक्त को अर्द्ध रक्त पर वरीयता प्राप्त होगी (Full blood will be preferred to half blood) – यदि सम्बन्ध अन्य मामलों में प्राकृतिक है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अनुसार पूर्ण रक्त सम्बन्ध के वारिस अर्द्ध रक्त सम्बन्ध के वारिसों पर उत्तराधिकार में वरीयता प्राप्त करेंगे अर्थात् पूर्ण रक्त सम्बन्ध के वारिसों की विद्यमानता (उपस्थिति) अर्द्ध रक्त सम्बन्ध के वारिसों को उत्तराधिकार से वंचित कर देगी। अपवर्जन का यह नियम एक समान पुरुष तथा स्त्री वारिसों पर लागू होगा। अधिमानता या वरीयता (Preference) का यह नियम उत्तराधिकार के क्रम (Order of Succession) को निर्धारित करने के प्रयोजन से लागू होगा।
भाई तथा बहन के अन्तर्गत पूर्ण रक्त या अद्ध रक्त के भाई बहन आते हैं। अतः अधिमानता या वरीयता के नियम के अनुसार पूर्ण रक्त के भाई बहन होने पर अर्द्ध रक्त का भाई या बहन उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह नियम मिताक्षरा विधि के अनुरूप है। यह नियम सिर्फ वहीं लागू होगा जहाँ स्पर्धा में पुरुष निर्वसीयती के पूर्ण रक्त भाई का पुत्र तथा अर्द्ध रक्त भाई या अर्द्ध रक्त बहन है। पूर्ण रक्त भाई का पुत्र द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों की तृतीय प्रविष्टि के अन्तर्गत आता है जबकि अर्द्ध रक्त भाई या अर्द्ध रक्त बहन द्वितीय प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं। अतः अर्द्ध रक्त के भाई या अर्द्ध रक्त की बहन को पूर्ण रक्त के भाई के पुत्र पर उत्तराधिकार में वरीयता या अधिमान प्राप्त होगा क्योंकि स्पर्द्धा विभिन्न वर्ग की प्रविष्टियों के मध्य है।
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ङ) द्वारा पूर्ण रक्त तथा अर्द्ध रक्त शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार दो व्यक्ति पूर्ण रक्त से सम्बन्धित तभी कहे जायेंगे जब वे सामान्य पूर्वज से एक ही पत्नी से उतरे हैं (descend), अर्द्ध रक्त सम्बन्धी • सामान्य पूर्वज की भिन्न पत्नियों से अवतरित हुए हैं। अ के पुत्र व तथा स पूर्ण रक्त हैं। अके भाई च का पुत्र अर्द्ध रक्त सम्बन्धी है।
(2) शाखावार तथा व्यक्तिवार उत्तराधिकार (Succession pre-stripe and per-capita)- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 19 यह प्रावधान करती है कि यदि निर्वसीयती सम्पत्ति के दो या दो से अधिक वारिस एक साथ उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं तो उनमें सम्पत्ति निम्न प्रकार से न्यागमित होगी-सम्पत्ति पायेंगे।
(क) इस अधिनियम में व्यक्तिवार (Pre-capita) न कि शाखावार (Per-stripe ) सम्पत्ति पायेंगे यदि इसके प्रतिकूल उपबन्ध न हो तो।
(ख) उत्तराधिकार सामान्य आसामियों (Tenant-in-common) के समान उत्तराधिकार पायेंगे न कि संयुक्त आसामी (Joint Tenant) की हैसियत से।
निर्वसीयती सम्पत्ति के व्यक्तिवार (Pre-capita) वितरण से तात्पर्य यह है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना अंश होता है तथा इस पर उसका अपना अधिकार है। उदाहरण के लिए जहाँ पुरुष निर्वसीयती के भाई, बहन, पुत्र की पुत्री का पुत्र तथा पुत्र के पुत्री के मध्य उत्तराधिकार का प्रश्न है ये सभी एक उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक समान अंश ग्रहण करेंगे।
शाखावार वितरण के मामले में दावेदार दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए अंश प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में पुरुष निर्वसीयती के वर्ग प्रथम के उसके वारिसों के मध्य सम्पत्ति वितरण के मामले में उत्तरजीवी पत्रों, पुत्रियों तथा माता, प्रत्येक एक अंश प्राप्त करेंगे जो व्यक्तिवार (Per-capita) वितरण हैं, जबकि पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की शाखा के वारिस आपस में धारा 10 के नियम 3 के अनुसार एक अंश ग्रहण करेंगे। इस प्रकार शाखावार वितरण में सम्पत्ति का वितरण प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
गर्भस्थ शिशु का अधिकार (Right of the child in womb ) – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 20 यह प्रावधान करती है कि यदि एक बच्चा निर्वसीयती पुरुष की मृत्यु के समय गर्भ में था तथा जो पश्चात्वर्ती समय में जीवित उत्पन्न होता है तो उसे निर्वसीयती के हित में वही अधिकार होंगे जैसे कि निर्वसीयती की मृत्यु के समय या मृत्यु के पूर्व बच्चे (शिशु) का जीवित रूप में जन्म हो चुका था तथा मान लिया जाता है कि निर्वसीयती पुरुष की मृत्यु की तिथि से ही ऐसे शिशु को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है जो निर्वसीयती पुरुष की मृत्यु के पूर्व गर्भ में आ गया था तथा जिसने निर्वसीयती पुरुष की मृत्यु के पश्चात् जीवित शिशु के रूप में जन्म लिया है। श्री डी० मुल्ला ने अपनी हिन्दू विधि की पुस्तक में भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं।
इस प्रकार इस धारा के अन्तर्गत गर्भस्थ शिशु को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त हो इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है –
(1) निर्वसीयती पुरुष सम्पत्तिधारक की मृत्यु के समय बच्चा गर्भ में आ गया था।
(2) पश्चात्वर्ती समय में बच्चा जीवित जन्म लेता है।
यदि उपरोक्त दो शर्तें पूरी हैं तो बच्चा या शिशु उसी प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करेगा जैसे कि निर्वसीयती सम्पत्तिधारक पुरुष को मृत्यु के समय (जिस समय उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न हुआ था) शिशु का जीवित अस्तित्व था। शिशु पुत्र हो या पुत्री इससे कोई अन्तर नहीं होता। गर्भस्थ शिशु उस व्यक्ति को उत्तराधिकार से बेदखल कर देता है जो उसके गर्भस्थ होने के दौरान सम्पत्ति को अस्थायी रूप से धारण करता है।
समसामयिक मृत्यु के मामले में उपधारणा (Presumption in case of Simuitaneous death)- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार जब दो व्यक्ति की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई हो जिनसे यह अनिश्चित हो कि उनमें से कौन पहले मरा अर्थात् यह अनिश्चित हो कि उसमें से कोई एक दूसरे का उत्तरजीवी रहा है या नहीं तथा कौन उत्तरजीवी रहा है वहाँ उत्तराधिकार सम्बन्धी सभी प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायेगी कि कनिष्ठ, ज्येष्ठ का उत्तराधिकारी रहा है। किसी दुर्घटना में जहाँ कई उत्तराधिकारी एक साथ मरते हैं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि उनमें से कौन पहले मरा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कनिष्ठ को ज्येष्ठ का उत्तरजीवी उपधारित करने का नियम बनाया गया। जैसे-पिता, पुत्र साथ-साथ मरते हैं तो यह उपधारणा होगी कि पिता पहले मरा तथा पुत्र उत्तरजीवी रहा। पिता क की सम्पत्ति में पुत्र ख उत्तराधिकार पायेगा तथा ख के पुत्र उसकी सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। कनिष्ठ से तात्पर्य सम्बन्ध में कनिष्ठ न कि उम्र में कनिष्ठ। यदि सम्बन्ध बराबर है (भाई-भाई) तो यहाँ उम्र कनिष्ठता का निर्धारण करने का आधार है। इन द मैटर ऑफ मातबर सिंह, ए० आई० आर० 1923 पंजाब 66 नामक बाद में गोलियों की बौछार में पति-पत्नी साथ-साथ मरे, पत्नी को पति का उत्तरजीवी माना गया। पुरानी हिन्दू विधि में ऐसा नियम नहीं था।
कुछ मामलों में सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिमानी (वरीयता) अधिकार (Preferential right to acquire property in certain cases) – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 यह प्रावधान करती है कि यदि अनुसूची के प्रथम श्रेणी (वर्ग) में उल्लिखित वारिसों में से कोई भी उत्तराधिकार की सम्पत्ति में अपने अंश का अन्तरण करना चाहता है तो अनुसूची के प्रथम श्रेणी में सन्दर्भित वारिसों में से किसी को सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार होगा अर्थात् सम्पत्ति में अंश अन्तरित करते समय अन्तरणकर्ता द्वारा वर्ग प्रथम के उत्तराधिकारियों को वरीयता देनी होगी।
इसी प्रकार के प्रावधान मुस्लिम विधि में भी हकशुफा (Pre-emption) के नाम से ज्ञात हैं। हकशुफा की भाँति यहाँ भी उत्तराधिकारियों के विक्रय तथा क्रय के अधिकार पर अवरोध खड़ा करता है। धारा 22 का प्रावधान सह-वारिसों के अधिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। अन्यथा हिन्दू विधि की प्रत्येक पवित्रता को खतरा था। धारा 22 के अन्तर्गत प्रावधानित नियम उन परिस्थितियों तक ही सीमित हैं जहाँ किसी सम्पत्ति के वर्ग प्रथम में दो या दो से अधिक वारिस हैं। अधिमानी या वरीयता के यह अधिकार पुरानी हिन्दू विधि की किसी स्मृति या श्रुति में नहीं मिलता। देश के कुछ भागों में यह नियम प्रथा के रूप में प्रचलित था।
अधिमानता या वरीयता के नियम के लागू होने के पूर्व निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है –
(1) यह अधिकार वर्ग प्रथम के वारिसों (Heirs) को प्राप्त है।
(2) यह अधिकार उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के अन्तरण के समय उत्पन्न होता है।
(3) सम्पत्ति के अन्तरण के पूर्व पक्षकारों के मध्य सम्पत्ति करार में प्रतिफल का अस्तित्व आवश्यक है।
(4) इस अधिकार का दावा न्यायालय में आवेदन देकर किया जा सकता है।
(5) ऐसे वारिस को अधिमानता दी जानी चाहिए जो अधिक मूल्य दे।
निवास स्थान (गृह) से सम्बन्धित विशेष प्रावधान ( Special Provision relating to dwelling houses) – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 निवास गृह (Dwelling Houses) के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान करती है। इस धारा में अनुसूची के वर्ग प्रथम के उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में प्राप्त निवास गृह (Dwelling House) के विभाजन को रोकने का अधिकार है। संयुक्त समिति की टिप्पणी के अनुसार जब तक पुरुष वारिस निवास गृह का विभाजन प्रभावी करने के विकल्प का चुनाव नहीं लेते स्त्री वारिस के विभाजन को प्रभावी करने के अधिकार पर धारा 23 प्रतिबन्ध लगाती है परन्तु यह धारा स्त्री वारिस के उस घर में निवास करने के अधिकार को अविभाज्य स्पष्ट रूप से मान्यता देती है।
धारा 23 के अनुसार- जहाँ एक निर्वसीयती हिन्दू अपने पीछे अनुसूची के प्रथम वर्ग में उल्लिखित किसी पुरुष या स्त्री वारिस को छोड़कर मरता है तथा उसकी सम्पत्ति में निवास गृह भी सम्मिलित है, (तथा निवास गृह) उसके परिवार के सदस्यों के आधिपत्य या कब्जे में है, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के रहते भी, ऐसी स्त्री वारिस का निवास गृह के विभाजन का दावा करने का अधिकार तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक पुरुष वारिस निवास गृह में अपने सम्बन्धित अंश के विभाजन का चुनाव न कर ले परन्तु स्त्री वारिस का उसमें निवास करने का अधिकार बना रहेगा। परन्तु यदि वह वारिस पुत्री है उसका निवास गृह में निवास करने का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक वह अविवाहित रहती है या उसका अभित्यजन (Desertion) कर दिया गया है या वह अपने पति से पृथक् हो गई है या वह स्त्री वारिस विषवा है।
धारा 23 निम्न शर्तों के पूरा होने पर ही लागू होगी-
(1) जहाँ पुरुष या स्त्री निर्वसीयत मरता है।
(2) पुरुष निर्वसीयती अपने पीछे पुरुष तथा स्त्री दोनों प्रकार के अनुसूची के वर्ग प्रथम में उल्लिखित वारिस छोड़कर मरता है। जहाँ निर्वसीयती के सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री वारिस हैं तथा वह अपने पीछे अनुसूची के द्वितीय श्रेणी के वारिस का अग्रज (Agentes) या बन्धु (Cognates) छोड़कर मरता है, यह धारा लागू नहीं होगी।
(3) निर्वसीयती की सम्पत्ति में उसके परिवार के सदस्यों के कब्जों में स्थित निवास गृह है। यदि सम्पत्ति में निवास गृह सम्मिलित नहीं है, सम्पत्ति का विभाजन हो सकता है। यदि निवास गृह परिवार के सदस्यों के पूर्ण आधिपत्य या कब्जे में नहीं है, विभाजन की माँग किये जाने पर कोई रुकावट नहीं है। यदि निवास गृह अंशत: निर्वसीयती के परिवार के सदस्यों के आधिपत्य में तथा अंशत: किरायेदार के आधिपत्य में हैं, यह धारा लागू नहीं होगी। वनिता बेन बालशंकर बनाम दिव्या बेन प्रेम जी, ए० आई० आर० 1979 गुजरात 116
किसी घर को निवास गृह माना जाय या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न तथा इसका निर्णय प्रत्येक वाद के तथ्य तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा धारा 23 को समाप्त कर दिया गया है। अतः अब पुत्रियाँ चाहे वह विवाहित हों अथवा अविवाहित हों, उन्हें मृतक के पुत्रों के समान पैतृक सम्पत्ति में रहने एवं विभाजन का पूर्ण अधिकार प्रदत्त कर दिया गया है।