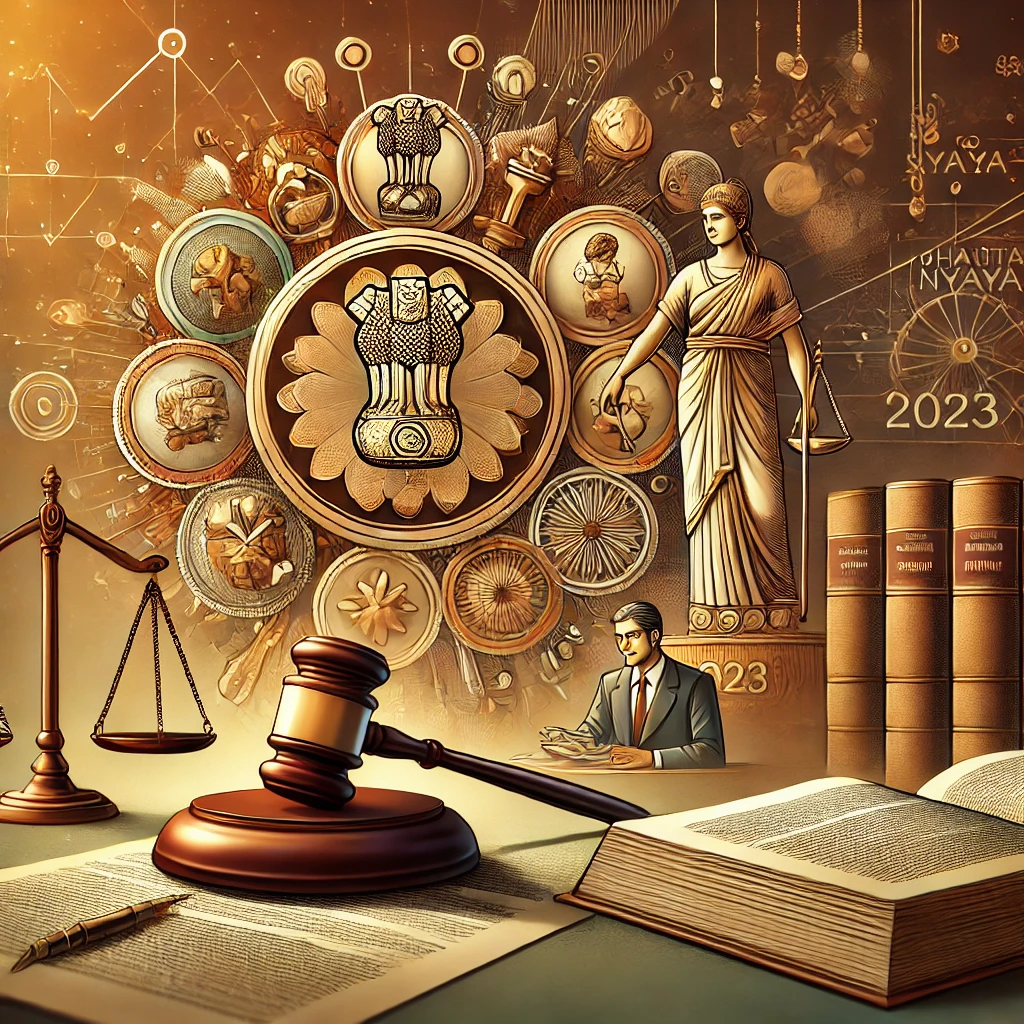“कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया: न्याय, समानता और विधिक वैधता के बीच संतुलन”
भूमिका
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि –
“किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।”
यह वाक्यांश भारतीय न्याय प्रणाली में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मूलधारा है। परंतु जब हम इस कथन पर विचार करते हैं कि “एक कानून, न्याय और समानता के सिद्धांतों से अलग होने के बावजूद, एक बार ठीक से अधिनियमित होने के बाद वैध रहता है”, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या मात्र वैधानिकता (legality) ही पर्याप्त है, या न्याय (justice) और नैतिकता (morality) भी जरूरी हैं?
‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) की व्याख्या
‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का अर्थ यह है कि यदि संसद या विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक विधिवत पारित किया गया है और उसे कानून का दर्जा मिल गया है, तो राज्य उस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष या नैतिक हो, केवल यह आवश्यक है कि वह विधिक रूप से पारित हुआ हो।
प्रारंभिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायपालिका ने शुरुआत में ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की संकीर्ण व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन बनाम राज्य मद्रास (1950) के ऐतिहासिक निर्णय में माना कि जब तक कोई कानून विधिवत पारित है, वह मान्य है – चाहे वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध क्यों न हो।
क्या यह सिद्धांत अन्यायपूर्ण कानून को वैध बना देता है?
यह सबसे बड़ा दार्शनिक और संवैधानिक प्रश्न है। यदि कोई कानून नृशंस, भेदभावपूर्ण या अमानवीय है लेकिन उसे विधिवत पारित किया गया है, तो क्या केवल इस आधार पर उसे संविधान सम्मत माना जाए?
इसका उत्तर सरल नहीं है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। परंतु ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का शाब्दिक अनुप्रयोग कई बार इन मूल्यों से विचलन कर सकता है।
‘Due Process of Law’ बनाम ‘Procedure Established by Law’
अमेरिकी संविधान में ‘Due Process of Law’ का सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि न केवल कानून विधिवत पारित हो, बल्कि वह न्यायसंगत, तार्किक और नैतिक रूप से उचित भी हो। भारत ने इस सिद्धांत को मूल रूप से ग्रहण नहीं किया था, लेकिन समय के साथ न्यायपालिका ने इसकी आत्मा को स्वीकार किया।
मानव अधिकारों और न्याय की कसौटी पर मूल्यांकन
यदि कोई कानून न्याय और समानता के विरुद्ध है, तो उसे केवल इसलिए स्वीकार कर लेना कि वह विधिवत पारित है, संविधान की आत्मा के विपरीत हो सकता है। कानून को न केवल वैध, बल्कि न्यायोचित भी होना चाहिए।
मनके गांधी बनाम भारत सरकार (1978): दृष्टिकोण में परिवर्तन
इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ‘Procedure Established by Law’ की व्याख्या करते हुए यह कहा कि –
“विधिक प्रक्रिया सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती; वह निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण होनी चाहिए।”
इस निर्णय ने ‘Due Process’ के तत्वों को भारतीय कानून में शामिल कर दिया।
संविधान के मूल ढांचे और न्याय का महत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ (social, economic and political justice) को प्रमुख स्थान दिया गया है। अतः कोई भी विधि, जो केवल अधिनियमित है परंतु अन्यायपूर्ण है, वह अंततः संविधान की आत्मा से टकरा सकती है।
उदाहरण के रूप में आपराधिक कानूनों की समीक्षा
कुछ पुराने आपराधिक कानून जैसे औपनिवेशिक युग के धारा 124A (राजद्रोह) या धारा 377 (समलैंगिकता पर प्रतिबंध) विधिवत अधिनियमित थे, परंतु समाज और न्याय के बदलते मूल्यों के साथ उन पर पुनर्विचार हुआ और न्यायालयों ने उन्हें निरस्त या अप्रभावी किया।
निष्कर्ष
“कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का यह अर्थ निकालना कि “एक बार कोई कानून अधिनियमित हो गया तो वह वैध है, चाहे वह न्याय के विरुद्ध ही क्यों न हो”, एक खतरनाक पूर्वग्रह हो सकता है।
संविधान का उद्देश्य केवल विधिक औपचारिकताओं को बनाए रखना नहीं है, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा जैसे मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है।
इसलिए आज आवश्यकता है कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को ‘न्याय द्वारा संचालित प्रक्रिया’ के रूप में व्याख्यायित किया जाए।