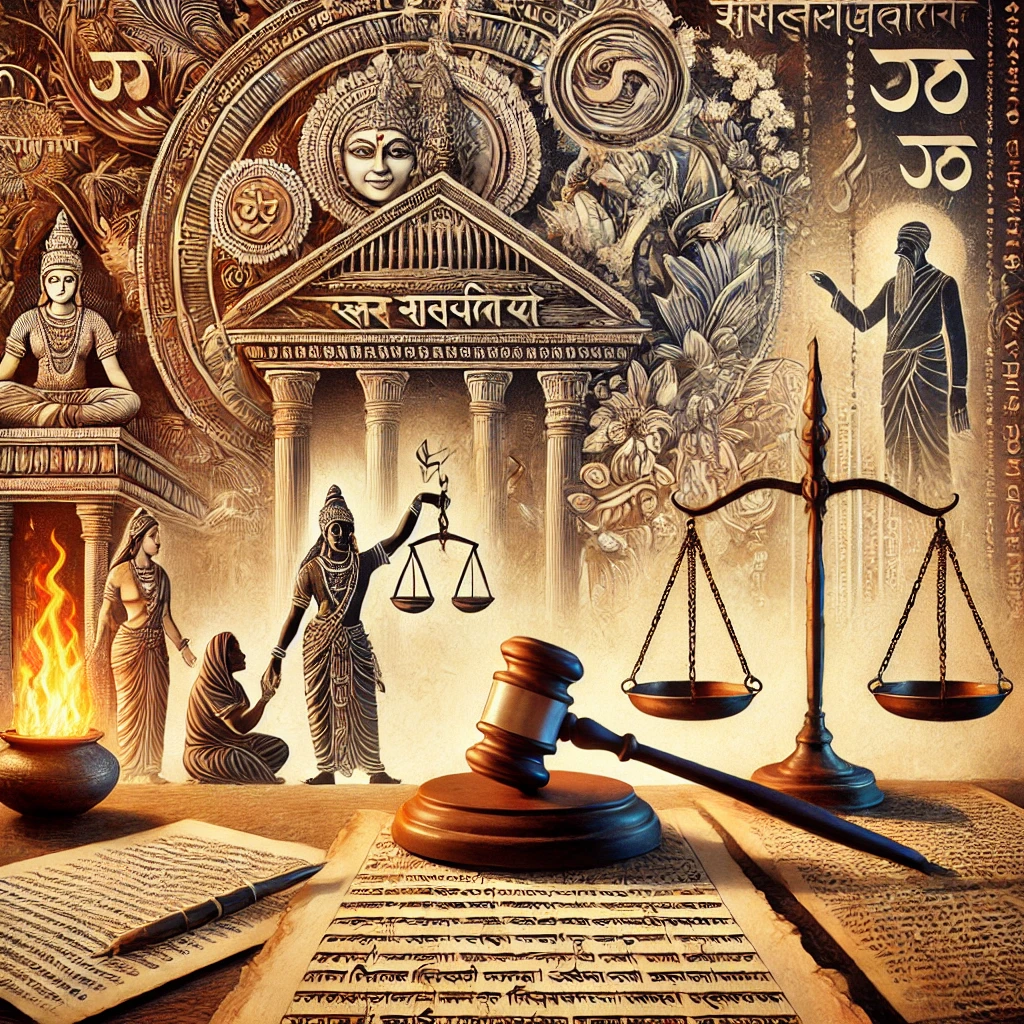प्रश्न 11. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी हिन्दू पुरुष या महिला के द्वारा किसी पुत्र या पुत्री के दत्तक ग्रहण के सामर्थ्य की विवेचना कीजिए।
Discuss the capacity of a male and female Hindu to adopt a son or daughter under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956
उत्तर– हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा-7 में द्वारा दत्तक ग्रहण का विधान किया गया है तथा वैध दत्तक ग्रहण के लिए सामर्थ्य तथा अधिकार दोनों का होना आवश्यक है।
हिन्दू पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण लेने की सामर्थ्य– धारा-7 के अनुसार कोई भी स्वस्थ चित्त वाला हिन्दू, यदि अवयस्क नहीं है, किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक ग्रहण में ले सकता है।
परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो जब तक कि पत्नी ने पूर्ण तथा अन्तिम रूप से संसार को त्याग न दिया हो अथवा हिन्दू न रह गई हो अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाली घोषित न कर दी गई हो तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण नहीं करेगा अर्थात् पत्नी अथवा पत्नियों की सहमति एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक बतायी गयी है। वर्तमान में पुत्र के अलावा पुत्री को भी दत्तक ग्रहण में लिया जा सकता है।
स्वस्थचित्तता तथा अवयस्कता– किसी भी हिन्दू पुरुष का दत्तक ग्रहण करने के योग्य होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं-(1) वह अवयस्क न हो, (2) वह स्वस्थ चित्त का हो ।
वर्तमान प्रावधान के अन्तर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व अवयस्कता की स्थिति मानी जायेगी। यानि वयस्कता की प्राप्ति 18 वर्ष के बाद ही की जा सकती है। स्वस्थ चित्त में तात्पर्य है कि दत्तक ग्रहण की प्रकृति से पूर्णतया वाकिफ हो।
पत्नी की सहमति – प्राचीन हिन्दू विधि में पत्नी की सहमति की आवश्यकता दत्तक ग्रहण करने के लिए नहीं थी, किन्तु वर्तमान अधिनियम में पत्नी या पलियों की सहमति को आवश्यक बताया गया है कि बिना उसके सहमति के वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार की सहमति के अभाव में दत्तक ग्रहण अमान्य समझा जायेगा।
एस० रम्मपा बनाम गुरुत्वा, ए० आई० आर० 2004 कर्नाटक 237 के बाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत पत्नी के मौजूद होने पर यदि पति दत्तक ग्रहण में कोई संतान लेता है तो उसके ग्रहण करने के पूर्व पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। इस प्रकार की सहमति के अभाव में कोई दत्तक ग्रहण अमान्य समझा जायेगा। निम्नलिखित दशाओं में सहमति आवश्यक नहीं है –
(1) यदि पत्नी पूर्व तथा अन्तिम रूप से संसार से विरक्त हो गई हो,
(2) वह हिन्दू नहीं रह गई हो, अथवा
(3) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क की घोषित की जा चुकी हो।
कृष्ण चन्द्र साहू बनाम प्रदीप्त दास, ए० आई० आर० 1982 उड़ीसा 114 के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पत्नी के संसार त्याग करने अथवा हिन्दू न रह जाने अथवा विकृत मस्तिष्क की घोषित न होने की बात नहीं कही जाती बिना उसकी सहमति के वैध दत्तक ग्रहण नहीं हो सकता। उपर्युक्त मामले में पत्नी की सहमति नहीं साबित को जा सको, अतएव न्यायालय ने दत्तक ग्रहण की अमान्य घोषित कर दिया।
ओलूराम बनाम रामलाल, ए० आई० आर० 1989 एम० पी० 198 के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि पत्नी अलग रह रही है अथवा घोर अनैतिक जीवन व्यतीत करती हुई कहीं अन्यत्र चली गई और वहाँ रहने लगी है तो इससे पुत्र को दत्तक ग्रहण में दिये जाने के सम्बन्ध में उसकी सहमति की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में यदि उसकी सहमति नहीं ली गई है तो दसक ग्रहण अवैध हो जायेगा।
जहाँ पति-पत्नी के मध्य न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति पास हो चुकी है, वहाँ भी पत्नी की सहमति के बिना पति दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि न्यायिक पृथक्करण से विवाह विच्छेद नहीं होता किन्तु शून्य विवाह के अन्तर्गत पत्नी की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस स्थिति में पत्नी एक वैध पत्नी नहीं होती है, अत: उसको सहमति आवश्यक नहीं है। पत्नी की सहमति स्पष्ट हो सकती है अथवा सांकेतिक सांकेतिक सहमति से तात्पर्य यह है कि यदि पत्नी ने दत्तक ग्रहण के अनुष्ठान में भाग न लिया हो, न उसका विरोध ही किया हो तो जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता कि वह दबाववश विरोध नहीं कर रही है, यह समझा जायेगा कि उसने अपनी सांकेतिक अनुमति दे दी है।
प्रफुल्ल कुमार बनाम शशि वेवा, AIR 1990 V.O.C. 13 के बाद में कहा गया कि जहाँ पत्नी ने दत्तक ग्रहण सम्बन्धी अनुष्ठान में पति के साथ भाग लिया है, वहाँ उसकी सहमति अवधारित कर ली जायेगी।
यदि किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हैं और यदि पुरुष अपनी पत्नियों की सहमति से एक पुत्र दत्तक लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी अन्य पत्नियाँ अलग-अलग सहमति देने के बाद भी दत्तक ले सकती हैं। इसे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है।
उदाहरण-‘ धर्मेन्द्र’ के तीन पत्नियाँ इना’ ‘मीना’ ‘डिका’ है ‘धर्मेन्द्र’ निस्संतान है। उसने तीनों पत्नियों की सहमति से एक पुत्र ‘ईव’ को दत्तक ग्रहण में लिया। ‘धर्मेन्द्र’ बाद में मर जाता है।’ धर्मेन्द्र’ के मरने के बाद ‘मीना’ तथा ‘डिका’ अलग-अलग एक-एक पुत्र ‘मन’ और ‘तन’ को दत्तक ग्रहण में लेती हैं। यहाँ ‘मन’ तथा ‘तन’ का दत्तक ग्रहण वैध है।
यदि किसी व्यक्ति के पुत्रों की मृत्यु हो जाय और वह निःसन्तान हो जाय तो क्या इसके पुत्रों की विधवा पत्नियों की उपस्थिति में वह व्यक्ति किसी पुत्र को दत्तक ग्रहण में ले सकता है?
हाँ दत्तक ग्रहण ले सकता है। इसे प्रफुल्लचन्द्र बनाम उड़ीसा राज्य, ए० आई० आर० 1988 उड़ीसा 18 के बाद में स्पष्ट किया गया। इसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि पुत्र-वधुओं की उपस्थिति उस व्यक्ति के दत्तक ग्रहण सम्बन्धी अधिकार पर बाधा नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति पुत्रों के मरने पर दूसरे पुत्र को दत्तक ग्रहण में ले सकता है हालाँकि उसके विधवा पुत्र-वधुओं को भी किसी सन्तान को दत्तक ग्रहण में लेने का अधिकार है।
स्त्रियों के दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य- इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को भी दत्तक ग्रहण करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, जिसमें उन्हें अब मत पति से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहीं। इस प्रकार का प्राधिकार पति से प्राप्त करना पूर्वविधि में आवश्यक था। अब अधिनियम में एक अविवाहिता स्त्री भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। एक स्त्री को दत्तक ग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 8 में निम्न बातों को आवश्यक बताया गया है –
(1) वह स्वस्थ चित्त की हो,
(2) वह अवयस्क न हो,
(3) वह विवाहिता न हो, अथवा
(4) यदि विवाहिता है तो उसने विवाह भंग कर दिया हो, अथवा
(5) (i) उसका पति मर चुका हो, अथवा
(ii) वह पूर्ण तथा अन्तिम रूप से संसार त्याग चुका हो, अथवा
(iii) उसका पति हिन्दू नहीं रह गया हो, अथवा
(iv) वह किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का घोषित किया जा चुका हो।
इस तरह हम देखते हैं कि स्त्रियों का दत्तक ग्रहण सम्बन्धी अधिकार सीमित है। यह अधिकार अविवाहितावस्था में अथवा विधवा होने की दशा में अथवा कुछ शर्तों के साथ विवाहित होने की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है।
जब दत्तक ग्रहण स्त्री द्वारा विवाहिता जीवन की स्थिति में किया जाता है तो वह सदैव पति के लिये होता है क्योंकि उस दशा में स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण तब किया जाता है जब पति धारा 8 के खण्ड (स) में दी गई किसी योग्यता से निर्योग्य हो चुका है। यदि स्त्री द्वारा विवाह के पूर्व अथवा वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाने के बाद दत्तक ग्रहण किया जाता है, इस प्रकार का सम्बन्ध चाहे मृत्यु द्वारा अथवा विवाह के भंग होने के कारण अथवा विवाह के अकृत एवं शून्य घोषित हो जाने के कारण समाप्त हुआ हो, तो उस दशा में स्त्री भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो पति को प्रभावित करता हो इसलिए स्त्री उसी दशा में पति के लिए दत्तक ग्रहण कर सकती है जब तक विवाहित जीवन की स्थिति बनी रहती है।
शून्य विवाह के अन्तर्गत, क्योंकि विवाह प्रारम्भतः शून्य होता है, पत्नी को यह अधिकार है कि वह पति के अधिकार के बिना दत्तक ग्रहण कर सकती है। ऐसे विवाह में उसकी स्थिति एक अविवाहिता स्त्री जैसी होती है। यद्यपि विवाह शून्य होता है फिर भी यदि उसके कोई पुत्र उस विवाह से उत्पन्न हो गया हो तो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अनुसार वह सन्तान वैध होगी और ऐसी सन्तान की उपस्थिति में वह सन्तानविहीन नहीं समझी जायेगी। अत: वह दत्तक ग्रहण भी नहीं कर सकती। तलाक हो जाने के बाद भी यदि पत्नी की कोई पुरुष अथवा स्त्री सन्तान रही हो तो वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जबकि एक हिन्दू स्त्री अनेक दत्तकग्रहीत सन्तानों को रख सकती है जो कि एक हिन्दू पुरुष के लिए सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ- एक अविवाहिता स्त्री ने एक पुत्र को दत्तक ग्रहण करने के पश्चात् विवाह कर लिया। पत्नी से सन्तान न होने पर पति ने एक दूसरा पुत्र दत्तक ग्रहण में लिया (जो कि वह कर सकता है, क्योंकि पत्नी के दत्तग्रहीत पुत्र का वह सौतेला पिता है)। इस प्रकार उस स्त्री के दो पुत्र हो गए।
दृष्टान्त–’वन्दना’ एक अविवाहिता स्त्री एक पुत्र ‘क’ को दत्तक ग्रहण में लेती है। कुछ समय बाद वह ‘स’ से विवाह कर लेती है। ‘स’ बाद में सन्तानहीन मर जाता है। ‘स’ के निमित्त ‘वन्दना’ अपने पूर्व दत्तक ग्रहीत पुत्र ‘क’ की उपस्थिति में एक दूसरे पुत्र ‘ख’ को दत्तक ग्रहण में लेती है। यहाँ दूसरे पुत्र ‘ख’ का दत्तक ग्रहण वैध होगा।
प्रश्न 12. (i) एक अवयस्क हिन्दू के नैसर्गिक (प्राकृतिक ) संरक्षक कौन हैं? उनकी शक्तियाँ क्या है? यदि एक अवयस्क का मिताक्षरा सहदायिकी के अन्तर्गत अविभाज्य अंश है तो क्या आपके उत्तर में कोई अन्तर पड़ेगा?
Who are natural guardian of a Hindu minor? What are their powers? Will it make any difference in your answer if such minor son has undivided interest in Mitakshara Coparcenary?
(ii) हिन्दू विवाह के अन्तर्गत एक संरक्षक को हटाने की परिस्थितियों एवं तरीकों की व्याख्या कीजिए।
How and when guardian under Hindu Law may be removed? Explain.
उत्तर (i) – प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian)– वह व्यक्ति जो अपने संव्यवहार स्वयं करने की विधिक क्षमता नहीं रखता, अवयस्क कहलाता है। कुछ निर्योग्यता (अवयस्कता, पागलपन आदि) के कारण व्यक्ति में अपने लिए संव्यवहार करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के हित के लिए संव्यवहार संरक्षक के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। प्राकृतिक संरक्षक वह व्यक्ति है जो अपने अवयस्क के साथ प्राकृतिक सम्बन्ध के कारण उसका संरक्षक हो जाता है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में संरक्षकता के विषय में अधिक नियम नहीं मिलते। नारद ने अपनी स्मृति में पिता और माता को संरक्षक बताया है।
अंग्रेजी शासन काल में स्ट्रेन्ज तथा मेकनाटन ने पिता, माता, बड़े भाई, अन्य पैतृक नातेदारों तथा उनके न रहने पर रिश्तेदारों को नैसर्गिक संरक्षक माना था।
परन्तु कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि किसी अजन्मे का नैसर्गिक संरक्षक उसका पिता उसके पश्चात् माता है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य नैसर्गिक संरक्षक नहीं है। सन् 1980 में संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम पारित करके न्यायालयों को संरक्षक नियुक्त करने के शक्ति दी गई।
सन् 1956 में हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम पारित करके संरक्षकता विषयक नियम को संहिताबद्ध कर दिया गया है। अब पिता, माता तथा पति को नैसर्गिक संरक्षक की कोटि में रखा गया है।
पिता तथा माता- पिता अपनी वैध सन्तान का (पुत्र या पुत्री का) नैसर्गिक संरक्षक है पिता के अतिरिक्त पिता के होने हुए कोई व्यक्ति नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकता। विवाहित पुत्रियों के विषय में उनके पति नैसर्गिक संरक्षक हैं। संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 19 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि पिता को उसकी नैसर्गिक संरक्षकता से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वह अनुपयुक्त न पाया जाय। इस कठोर नियम को हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 द्वारा कुछ लचीला बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान किया गया है कि अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि है तथा पिता की संरक्षकता तथा अभिरक्षा का अधिकार इस नियम के अधीन है।
हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के पूर्व पिता अपनी वसीयत के माध्यम से माता के नैसर्गिक संरक्षक के अधिकार को समाप्त करके अन्य व्यक्ति को वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार रखता था, परन्तु अब यदि पिता की मृत्यु के पश्चात् माता जीवित है तो पिता द्वारा नियुक्त किया गया वसीयती संरक्षक प्रभावी नहीं होगा। धारा 9 (2) के अनुसार यदि माता वसीयती संरक्षक नियुक्त किये बिना मर जाती है तो पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक प्रभावी होगा परन्तु यदि माता अपना वसीयती संरक्षक नियुक्त करके मरती है तो उसके पति द्वारा नियुक्त संरक्षक प्रभावी होगा। इस प्रकार पष्ट है कि तथा पिता अपने अवयस्क पुत्र के लिए वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। परन्तु माता के जीवित रहने तक पिता तथा उसके पश्चात् माता नैसर्गिक संरक्षक है। हमारे यहाँ संयुक्त संरक्षक का प्रावधान नहीं है। नैसर्गिक संरक्षकता के विषय में पुत्र तथा दत्तक के बारे में नियम एक समान है। अधर्मज (अवैध) सन्तान के बारे में माता के जीवन काल में माता हो नैसर्गिक संरक्षक है उसके पश्चात् पिता अधर्मज सन्तान का नैसर्गिक संरक्षक है।
जीजाबाई बनाम पठान, (1971) के मामले में यह प्रश्न उठा कि यदि पिता अपने पुत्र के संरक्षण में उदासीनता, निष्क्रियता दिखाता है तो क्या पिता के जीवित रहते माता नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है? इस बाद में एक अवयस्क के माता-पिता 20 वर्षों से अलग रहते थे। इस काल में माता ही पुत्री की देखभाल तथा पालन करती थी। पिता पुत्री की देखभाल के प्रति बिल्कुल उदासीन था। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वैद्यलिंगम ने कहा कि ऐसी स्थिति में नैसर्गिक संरक्षक की समस्त शक्तियों तथा अधिकारों का प्रयोग माता नैसर्गिक संरक्षक की तरह कर सकती थी।
इस बाद के निर्णय से स्पष्ट है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ही पिता के जीवित रहते माता नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 (क) के परन्तुक के अनुसार सामान्यतः पाँच वर्ष की आयु तक सन्तान की अभिरक्षा माता में निहित रहती है यद्यपि पिता ही सन्तान का संरक्षक बना रहेगा।
गायत्री बजाज बनाम जीतिन भल्ला, ए० आई० आर० (2013) एस० जी० 10 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि न्यायालय ने पत्नी की याचिका को निरस्त करते हुए यह निर्णीत किया कि बच्चों का भविष्य पिता की अभिरक्षा में ज्यादा सुरक्षित है, और जहाँ सन्तान अपने पिता के साथ ही रहना चाहती है वहाँ माता को अपनी सन्तान को अपने साथ रखने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसे ऐसी परिस्थिति में उसे मिलने एवं सम्पर्क बनाये रखने का ही अधिकार होगा।
एक अधर्मज सन्तान के मामले में पिता के जीवनकाल में भी माता ही संरक्षक होती है। परन्तु मौतेले माता-पिता न तो नैसर्गिक संरक्षक हो सकते हैं न हो अन्य प्रकार के विधिक संरक्षक जब तक न्यायालय उन्हें संरक्षक नियुक्त न कर दे। इस प्रकार सौतेले माता-पिता के मामले में माता-पिता न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक कहलायेंगे न कि नैसर्गिक संरक्षक।
पति– हिन्दू स्मृतियों, टीकाओं तथा निबन्ध में इस विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है परन्तु संसार की कुछ विधि व्यवस्थाओं में अवयस्क पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक पति को हो माना गया है। प्राचीन तथा आधुनिक हिन्दू विधि में भी यही नियम है। मनु के अनुसार स्त्री कभी भी स्वतन्त्र नहीं है। बाल्यकाल में उसका पिता, दाम्पत्य काल में उसका पति तथा वृद्धावस्था (विधवाकाल) में उसका पुत्र उसका संरक्षक होता है। संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत जब तक पति अनुपयुक्त न पाया जाय, उसे पत्नी की नैसर्गिक संरक्षकता से नहीं हटाया जा सकता। न्यायालयों ने इस नियम को पत्नी के कल्याण के अधीन माना है। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम के अन्तर्गत पति-पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक है। परन्तु इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यह नियम भी स्त्री के कल्याण के लिए है।
इस प्रकार हम कह सकते है कि सन्तान का नैसर्गिक संरक्षक उसका पिता है। पिता के न रहने पर उसकी माता उसकी नैसर्गिक संरक्षक है। धर्मज (Legitimate) सन्तान तथा दत्तक सन्तान के बारे में एक ही नियम है। परन्तु अधर्मज सन्तान को नैसर्गिक संरक्षक उसको माता है। सौतेले माता-पिता के मामले में यह नियम है कि सौतेले माता-पिता नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकते परन्तु न्यायालय उन्हें सन्तान का संरक्षक नियुक्त कर सकती हैं। विवाहित स्त्री के मामले में यह मान्य नियम है कि पति ही उसका नैसर्गिक संरक्षक है। परन्तु भारत जैसे देश में जहाँ बाल विवाह का बोलबाला है, एक विवाहित बालिका के हित तथा कल्याण में यह उत्तम होगा कि पति, पत्नी की संरक्षकता तब तक प्राप्त न करे जब तक कि बालिका मैथुन योग्य न हो जाय। एक विवाहित बालिका के मैथुन योग्य होने तक उसकी माता को नैसर्गिक संरक्षक बनाने हेतु नियम बनाना स्वागत योग्य होगा क्योंकि माता-पिता ही अपनी अवयस्क बालिका (विवाहित या अविवाहित) का सबसे अधिक कल्याण सोच सकता है।
नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ (Powers of Natural Guardian )- हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 एक अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में प्रावधान करती है।
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार नैसर्गिक संरक्षक उन सभी कृत्यों के सम्पादन का अधिकारी होगा जो अवयस्क की सम्पत्ति की सुरक्षा, संरक्षण तथा कल्याण के लिए आवश्यक तथा (उपयुक्त) युक्तियुक्त (Necessary and reasonable) हो। परन्तु किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत संव्यवहारों में नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क को बाँध नहीं सकता अर्थात् व्यक्तिगत संव्यवहारों के माध्यम से एक नैसर्गिक संरक्षक को अवयस्क पर दायित्व डालने का अधिकार नहीं होगा। धारा 8 के अन्तर्गत प्रदत्त यह शक्ति अति व्यापक है जिसके अन्तर्गत नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है जो आवश्यक तथा उपयुक्त है। अवयस्क के कल्याण के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
अवयस्क की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित शक्तियाँ (Powers relating to alienation (transfer) of Immovable property of minor (ward) – हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के लागू होने के पूर्व एक नैसर्गिक संरक्षक (Natural Guardian) को अपने अपत्य अवयस्क की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित असीमित अधिकार था। एक नैसर्गिक संरक्षक अपने अपत्य अवयस्क की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण उसके कल्याण या आवश्यकताओं के लिए कर सकता था। उसकी शक्तियाँ संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता (Karta) की भाँति थीं। अवयस्क का कल्याण तथा अवयस्क की आवश्यकता का मानक या मापदण्ड का निर्धारण नैसर्गिक संरक्षक स्वयं करता था। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के पारित होने के पश्चात नैसर्गिक संरक्षक के उक्त अधिकार या शक्ति में मौलिक परिवर्तन यह आया कि अब अवयस्क की आवश्यकता तथा कल्याण क्या है, इसका मानक तथा मापदण्ड निर्धारित करने का अधिकार निष्पक्ष न्यायालय को प्रदान किया गया है। अब नैसर्गिक संरक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अवयस्क (अपत्य) की अचल सम्पत्ति के संव्यवहार के पूर्व न्यायालय की अनुमति आवश्यक रूप से ले।
एक नैसर्गिक संरक्षक – (1) न्यायालय की अनुमति के बिना अवयस्क (अपत्य) की अचल सम्पत्ति का किसी भी भाँति अंतरण या हस्तान्तरण नहीं कर सकता तथा वह अपत्य (अवयस्क) की सम्पत्ति को पाँच वर्ष की अवधि के या अपत्य (Ward) के वयस्क होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिए पट्टे (lease) पर नहीं दे सकता। [धारा 8 (2) ] ।
न्यायालय यह अनुमति तभी देगा जब ऐसा हस्तान्तरण अवयस्क या अपत्य (Ward) के कल्याण के लिए आवश्यक है तथा अवयस्क या अपत्य के प्रत्यक्ष लाभ के लिए है। [धारा 8 (4)]।
न्यायालय की अनुमति के अभाव में नैसर्गिक संरक्षक द्वारा अवयस्क या अपत्य को अचल सम्पत्ति का किया गया अन्तरण अवयस्क या अपत्य की स्वेच्छा (discretion) पर शून्य (Void) होगा। इसके लिए आवेदन अवयस्क या अन्य कोई व्यक्ति भी दे सकता है जो इस हस्तान्तरण से प्रभावित हो [धारा 8 (3) ]
वर्तमान हिन्दू विधि में नैसर्गिक संरक्षक (Natural Guardian) की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 (4) में प्रयुक्त आवश्यकता तथा कल्याण (प्रसुविधा) शब्दों का अर्थ हिन्दू विधि में प्रयुक्त वैध आवश्यकता तथा सम्पत्ति की प्रसुविधा (कल्याण) शब्द से विस्तृत है तथा न्यायालय इन शब्दों की व्याख्या करने के लिए स्वतन्त्र है।
इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या अन्तरिती (Transferee) (जिसको अवयस्क की अचल सम्पत्ति अन्तरित की गई है) यह कहकर अपने कृत्य । उचित ठहरा सकता है। कि उसने सद्भावपूर्वक जाँच की थी तथा अन्तरण अवयस्क की आवश्यकता तथा सम्पत्ति के कल्याण के लिए वास्तव में था या नहीं इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। यह नियम मनराज कुंवर के वाद में प्रतिपादित किया गया है। विधि विद्वान डेरेक का विचार इस नियम को बनाये रखने के पक्ष में हैं।
अवयस्क या अपत्य की चल सम्पत्ति (Movable property) के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। इस सम्बन्ध में नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ वही हैं जो इस विधेयक के लागू होने के पूर्व थीं।
अवयस्क या अपत्य की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संरक्षक तथा पाल्य अधिनियम (Guardian and Wards Act), 1890 के प्रावधान लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का निरूपण संरक्षक तथा पाल्य अधिनियम, 1890 की धाराएँ 27, 29, 31, 32 तथा 33 महत्वपूर्ण हैं। प्रक्रिया का निरूपण इस अधिनियम की धारा 31 उपधारा (2), (3) तथा (4) में किया गया है।
यदि न्यायालय सम्पत्ति के अन्तरण की अनुमति देने से इन्कार कर देती है तो इसकी अपील उस न्यायालय में की जा सकेगी जिस न्यायालय में उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती जिसने अनुमति देने से इन्कार किया है।
इस धारा में न्यायालय का तात्पर्य शहर की दीवानी न्यायालय (Civil Courts) या जिला न्यायालय से है। अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए आवेदन उस जिला या दीवानी न्यायालय में किया जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह सम्पत्ति स्थित हो।
न्यायालय की अनुमति के अभाव में किये गये हस्तान्तरण का प्रभाव – न्यायालय की अनुमति के अभाव में या अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक अवयस्क या अपत्य की अचल सम्पत्ति का किया गया हस्तान्तरण अवयस्क या अपत्य के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा अर्थात् यह हस्तान्तरण तब तक शून्य नहीं होगा जब तक उसके विरुद्ध अपत्य या अवयस्क ने आपत्ति न की हो। इस विषय में आपत्ति अवयस्क द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो अवयस्क की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित है।
इस सम्बन्ध में दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं –
(1) यदि अवयस्क द्वारा अन्तरण को रद्द कराया जाता है तो क्या अचल सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त मूल्य अवयस्क या अपत्य द्वारा लौटाया जाना आवश्यक है। यह सुस्थापित नियम है कि अपत्य को यह मूल्य लौटाना होगा। [जनार्दन बनाम भगवती कुट्टी, ए० आई० आर० 1988 केरल 303]
(2) क्या हस्तान्तरण को रद्द कराने हेतु अवयस्क द्वारा वाद दायर करना होगा या अन्तरण स्वयं रद्द होगा। इस प्रश्न पर हमारे न्यायालय के विचारों में मतभेद है। परन्तु निम्न दो नियम स्थापित माने जा सकते हैं –
(i) यदि अपत्य या अवयस्क अन्तरण की गई सम्पत्ति पर कब्जा पाना चाहता है. तो उसे अन्तरण को रद्द करवाने हेतु वाद लाना होगा।
(ii) यदि अपत्य या अवयस्क की सम्पत्ति पर अवयस्क का कब्जा है तो उसे अन्तरण को रद्द करने हेतु वाद लाना आवश्यक नहीं है।
यह स्मरणीय है कि अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 नैसर्गिक संरक्षक के चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में तथा करार (अनुबन्ध Agreement) करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता।
बघेला बनाम मसुलद्दीन, (1887) 11 मुम्बई 218 सरवरजान बनाम फखरुद्दीन, (1912) 39 इण्डियन अपील नामक वादों में प्रिवी कौंसिल के निर्णयों से यह मत सुनिश्चित हो गया है कि नैसर्गिक संरक्षक अनुबन्धों (Agreements) द्वारा अवयस्क या अपत्य की सम्पत्ति को आबद्ध कर सकता है परन्तु अवयस्क या अपत्य को व्यक्तिगत रूप से आवद्ध नहीं कर सकता। यह पूर्णतया स्थापित नियम है कि नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क या अपत्य की और से सगाई तथा विवाह के अनुबन्ध या प्रशिक्षुता (Apprenticeship) के अनुबन्ध कर सकता है। इसी भाँति नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की ओर से कौटुम्बिक प्रबन्ध (Family arrangement) भी कर सकता है। संरक्षक, अनुबन्ध द्वारा अवयस्क को उन ऋणों के लिए उत्तरदायों ठहरा सकता है जो अवयस्क की आवश्यक वस्तुओं के लिए लिया गया है। न्यायालय इस विचार पर एक मत है कि अपत्य उन ऋणों के लिए उत्तरदायी है जिनके अन्तर्गत संरक्षक स्वयं उत्तरदायी है। यदि संरक्षक किसी परक्राम्य लिखत (Negotiable instrument) पर स्वयं उत्तरदायी है तो अवयस्क या अपत्य भी उस परक्राम्य लिखत पर उत्तरदायी होगा।
क्रय-विक्रय का अनुबन्ध तथा करार का विनिर्दिष्ट पालन- इस विषय में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संरक्षक क्रय विक्रय के अनुबन्ध द्वारा अवयस्क की सम्पत्ति को दायी ठहरा सकता है यदि हाँ तो क्या ऐसे अनुबन्ध का विनिर्दिष्ट अनुपालन (Specific (performance) कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायालयों ने सम्पत्ति के क्रय तथा विक्रय के संव्यवहार में भेद किया है। न्यायालयों का बहुमत इस पक्ष में है कि संरक्षक को अपत्य (अवयस्क) के लिए सम्पत्ति क्रय करने का अनुबन्ध करने की शक्ति है परन्तु वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के अभाव में अवयस्क की सम्पत्ति को विक्रय करने का अनुबन्ध करने की शक्ति नहीं रखता। न्यायालय इस विचार के हैं कि संरक्षक के द्वारा किये गये अनुबन्ध का विनिर्दिष्ट पालन भी कराया जा सकता है।
अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 उस अवयस्क को इस अधिनियम के प्रवर्तन (Enforcement) से मुक्त करता है जिसका संयुक्त हिन्दू परिवार में अविभाज्य अंश है तथा जिसका इस अधिनियम में परिभाषित नैसर्गिक संरक्षक है। अतः यह स्पष्ट है कि एक ऐसे अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक, जिसका संयुक्त परिवार में अविभाज्य अंश है, पर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित इस अधिनियम की धारा 8 (2) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध लागू नहीं होते। इसका परिणाम यह होगा कि जब तक हिन्दू विधि लागू है एक पिता, जो एक नैसर्गिक संरक्षक है, सहदायिकी सम्पत्ति (Coparcenary Property) में (संयुक्त परिवार में) अवयस्क के अविभाज्य अंश में अवयस्क के हित का अन्तरण कर सकता है परन्तु इस शक्ति या अन्तरण के अधिकार पर हिन्दू विधि के अन्तर्गत प्रावधान लागू होंगे अर्थात् एक नैसर्गिक संरक्षक हिन्दू अवयस्क के संयुक्त परिवार में अविभाज्य अंश का अन्तरण अवयस्क की परिसम्पत्ति के प्रलाभ के लिए तथा वैध आवश्यकता के लिए कर सकता है। यहाँ न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन दोनों प्रावधानों में अन्तर यह है कि अधिनियम की धारा 8 (2) के अन्तर्गत अवयस्क की सम्पत्ति के अन्तरण के लिए उस शहर के दीवानी न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है जिसके क्षेत्राधिकार में अवयस्क की अचल सम्पत्ति या उसका अंश स्थित है। जबकि हिन्दू विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति के लाभ तथा विधिक आवश्यकता के लिए नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की अचल सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है। (अरुन कुमार बनाम चन्द्रावती, ए० आई० आर० 1978 इलाहाबाद 221)। इन प्रावधानों में मौलिक अन्तर यह है कि हिन्दू विधि में अचल सम्पत्ति का लाभ तथा अवयस्क को आवश्यकता क्या है, यह निर्णय करना संरक्षक का विवेक था जबकि अब अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति का लाभ तथा अवयस्क की आवश्यकता क्या है. इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है। अवयस्क विधिक आवश्यकता तथा सम्पत्ति का लाभ क्या है यह विलेख में निरूपण की विषय वस्तु नहीं है। इसे चुनौती देने पर न्यायालय में कठोरतापूर्वक साबित किया जाना आश्वश्यक है।
यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के लागू होने के पूर्व नैसर्गिक संरक्षक की अवयस्क की अचल सम्पत्ति के अन्तरण की शक्ति काफी विस्तृत थी। हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई, (1956) 6 एम० आई० ए० 398 नामक बाद में प्रिवी काउन्सिल ने यह स्पष्ट किया कि अवयस्क की वैध आवश्यकताओं के लिए नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति को बन्धक रख सकता था, विक्रय कर सकता था, उस पर प्रभार (charge) या दायित्व डाल सकता था या उसको किसी भी प्रकार से अन्तरित कर सकता था। परन्तु इस अन्तरण को चुनौती दिये जाने पर नैसर्गिक संरक्षक को यह साबित करना होता था कि यह अन्तरण अवयस्क की अचल सम्पत्ति या अवयस्क की विधिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक था।
सम्पत्ति का प्रलाभ या अवयस्क की वैध आवश्यकता क्या है यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों पर निर्भर करता था।
पी० टी० चाधु चेट्टीयार बनाम करियत कनुम्मल कानारन, ए० आई० आर० 1984 केरल 118 नामक बाद में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक पिता जीवित है या उसे न्यायालय द्वारा नैसर्गिक संरक्षक के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, माता अवयस्क की नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकती तथा वह अवयस्क की अचल सम्पत्ति का अन्तरण नहीं कर सकती तथा उसके द्वारा अवयस्क की सम्पत्ति का किसी प्रकार का अन्तरण अवैध तथा किसी विधिक प्रभाव का नहीं होगा।
उत्तर (ii)–संरक्षक होने की अयोग्यतायें– हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में कोई व्यक्ति संरक्षक बनने के अयोग्य हो जाता है –
(1) धर्म परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता:
(ii) सिविल मृत्यु से उत्पन्न अयोग्यता;
(iii) अवयस्कता से उत्पन्न अयोग्यता;
(iv) जब संरक्षकता अवयस्क के कल्याण के लिए नहीं है।
(1) धर्म परिवर्तन- इस अधिनियम के पास होने के पूर्व धर्म परिवर्तन से संरक्षक के अधिकार नहीं प्रभावित होते थे। इस बात से कि पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसके पुत्र की अभिरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता था। किन्तु यदि धर्म परिवर्तन के समय पिता ने स्वेच्छा से इस प्रकार के पैतृक अधिकार को त्याग दिया और पुत्र को अभिरक्षा को दूसरे के हाथ सौंप दिया है तो उस दशा में न्यायालय पुत्र की अभिरक्षा को पिता के हाथ में नहीं दें सकता, यदि यह पुत्र के हितों के विपरीत है। किन्तु जहाँ किसी हिन्दू माता ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वहाँ न्यायालय पुत्र को माता को अभिरक्षा से हटाकर किसी एक हिन्दू संरक्षक के अधीन कर सकता है, यदि वह अवयस्क के हितों के अनुकूल हो। इसी प्रकार जहाँ पत्नी ने विवाह-विच्छेद करके किसी दूसरे धर्मावलम्बी के साथ विवाह कर लिया, उससे अपने पुत्र को अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।
वर्तमान अधिनियम द्वारा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये हैं। अधिनियम द्वारा विहित कोई भी प्राकृतिक संरक्षक अर्थात् पिता, माता अथवा पति के हिन्दू न रह जाने पर संरक्षक बनने का अधिकार नहीं रह जाता। विजय लक्ष्मी बनाम पुलिस इंस्पेक्टर, ए० आई० आर० (1991) मद्रास के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पिता इस्लाम धर्म को स्वीकार करके एक मुस्लिम महिला से विवाह कर लेता है वहाँ वह नैसर्गिक संरक्षक होने का विधिक अधिकारी नहीं रह जाता।
(2) सिविल मृत्यु (Civil Death)- कोई भी व्यक्ति जिसने पूर्णतया अन्तिम रूप से संसार त्याग दिया है अथवा यती अथवा संन्यासी हो चुका है, वह अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक होने का अधिकारी नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति संन्यासी अथवा यती कह देने मात्र से संन्यासी या यती नहीं हो जाता। संसार का त्याग यथाथी रूप में पूर्णतया अन्तिम होना चाहिए।
”वह व्यक्ति जो संन्यासी अथवा यती होने की इच्छा करता है, उसे अपना मृत्यु संस्कार तथा श्राद्ध विधिवत् करना चाहिए तथा अपनी सभी सम्पत्ति को अपने पुत्रों तथा ब्राह्मणों में विभाजित कर देना चाहिए। उसके पश्चात् होम आदि की क्रिया करके जल में खड़ा होकर उस उद्देश्य का मंत्र तीन बार पढ़ना चाहिए कि उसने संसार की समस्त वस्तुएँ, पुत्र तथा सम्पत्ति आदि को त्याग दिया। [शीला बनाम जीवन लाल, ए० आई० आर० (1988) ए० पी०] [275]।
(3) अवयस्कता – अधिनियम की धारा 10 में यह विहित किया गया है कि कोई अवयस्क किसी अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में संरक्षक बनने के अयोग्य है।
(4) अवयस्क के कल्याण के प्रतिकूल– कोई भी ऐसा व्यक्ति संरक्षक नहीं बन सकता जिसकी संरक्षकता न्यायालय की दृष्टि में अवयस्क के कल्याण के विपरीत होगी। धारा 13 के अन्तर्गत अवयस्क के कल्याण को सर्वोपरिता दी गई है। अतएव अवयस्क की संरक्षकता उसके कल्याण की अनुकूलता के आधार पर की जायेगी। श्रीमती गंगाबाई बनाम भेरूलाल, ए० आई० आर० 1976 राजस्थान 153 के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहा कि विधि में पिता एक प्राकृतिक संरक्षक होता है तथा सामान्यतः उसे पुत्र को अपने साथ रखने के प्राकृतिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि न्यायालय को एक भिन्न विचारधारा धारण करनी पड़ती है जबकि पिता को एक प्राकृतिक संरक्षक होने के बावजूद अवयस्क को उसकी संरक्षकता में नहीं दिया जा सकता। यदि पिता की संरक्षकता में संतान का कल्याण खतरे में प्रतीत हो तथा माता की संरक्षकता में उसका कल्याण समान रूप से अथवा अधिक मात्रा में प्रतीत हो तो पिता अवयस्क के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
विनोद चन्द बनाम श्रीमती अनुपमा, ए आई० आर० (1993) बाम्बे 232 के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने पिता को अपनी अवयस्क सन्तान से मिलने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। पिता ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अपनी अवयस्क सन्तान को, जो माता के साथ रहती थी, चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से गुजारे की राशि के रूप में प्रदान नहीं कर रहा था। न्यायालय ने कहा कि जब तक पिता न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे अपनी सन्तान के पास पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्रश्न 13. हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम में वसीयती संरक्षक सम्बन्धी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उनकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। किन परिस्थितियों में उसे हटाया जा सकता है।
Discuss in detail the provisions regarding testamentary guardian under Hindu Minority and Guardianship Act. Discuss the powers of testamentary guardian. On what grounds he can be removed.
उत्तर – अवयस्क व्यक्ति अपने लिए संविदा करने का अधिकार या क्षमता नहीं रखता। परन्तु अवयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविदा की अनिवार्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विधि यह अनुमति देती है कि अवयस्क के लिए संविदा या अन्य विधिक कार्य उसके संरक्षक के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 में वसीयती संरक्षक की नियुक्ति का अधिकार माता तथा पिता दोनों को धारा 9 द्वारा प्रदान किया गया है।
एक अवयस्क के वसीयतो संरक्षक वे संरक्षक हैं जो उन प्राकृतिक या नैसर्गिक संरक्षकों की वसीयत द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है। वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावी होती है।
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 पारित होने से पूर्व ऐसा प्रतीत होता है कि संरक्षक की नियुक्ति वसीयत द्वारा या अन्य किसी वसीयती सम्पत्ति अन्तरण के दस्तावेज द्वारा की जा सकती थी, परन्तु अब हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत वसीयती संरक्षक की नियुक्ति सिर्फ वसीयत द्वारा ही की जा सकती है।
वसीयती संरक्षक किसे नियुक्त किया जा सकता है?
(1) एक हिन्दू पिता अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है तथा एक हिन्दू पिता को (यदि वह सन्यास या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर नैसर्गिक संरक्षक की क्षमता नहीं रखे है) अपने औरस अवयस्क सन्तान के लिए अवयस्क की देखभाल के लिए वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति है। यह संरक्षक अवयस्क के शरीर (भरण-पोषण) तथा सम्पत्ति दोनों के लिए नियुक्त हो सकता है।
(2) यदि पिता ने अपनी वसीयत में संरक्षक की नियुक्ति तो की है, परन्तु वह यदि अवयस्क की माता के पहले मर जाता है तो वसीयत में नियुक्त संरक्षक वसीयती एवं नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य इसलिए नहीं करेगा क्योंकि माता के रूप में नैसर्गिक संरक्षक जीवित है। यदि माता बिना किसी वसीयती संरक्षक को नियुक्त किये मर जाती है तब उस परिस्थिति में पिता द्वारा अपनी वसीयत में नियुक्त वसीयती संरक्षक नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
(3) एक हिन्दू विधवा को अपने धर्मज अवयस्क बच्चों के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार है अत: एक विधवा माता को वसीयत द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। यह उल्लेखनीय है कि यदि एक हिन्दू पिता अपने धर्मज सन्तान के लिए किसी कारण से (असमर्थ होने के कारण) नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो पिता के जीवनकाल में ही माता नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी तथा वसीयत द्वारा अपने अवयस्क धर्मज सन्तान के शरीर तथा सम्पत्ति दोनों के लिए वसीयतो संरक्षक नियुक्त करने में सक्षम है।
(4) एक हिन्दू माता को अपने अधर्मज बच्चों के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार एक हिन्दू माता अपने अधर्मज सन्तान को सम्पत्ति तथा शरीर के लिए वसीयत द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार रखती है।
इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि एक हिन्दू पिता अपने अवयस्क धर्मज सन्तान का नैसर्गिक संरक्षक है तथा उसे वह वसीयत द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है. परन्तु यदि पिता का देहान्त माता के जीवनकाल में हो जाता है तो पिता द्वारा वसीयती संरक्षक प्रभावी नहीं होगा परन्तु माता ही नैसर्गिक संरक्षक होगी और माता को भी वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। यदि माता-पिता की अनुपस्थिति या अक्षमता पर (सन्यासी पति या वानप्रस्थी होने पर) नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है तो उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थिति में माता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक ही प्रभावी होगा न कि पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक। परन्तु यदि किसी मामले में पिता ने वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त किया है तथा वह माता से पूर्व मर जाता है या अक्षम हो जाता है और माता ने कोई वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं किया है तो पिता द्वारा वसीयत के माध्यम से नियुक्त वसोयती संरक्षक अवयस्क बच्चे के शरीर तथा सम्पत्ति के लिए नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार एक अधर्मज सन्तान के सम्बन्ध में उसकी माता ही नैसर्गिक संरक्षक होगी तथा वह वसीयत द्वारा अपने अधर्मज सन्तान का संरक्षक पिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर पिता को नैसर्गिक संरक्षक होने से वंचित कर सकती है।
वसीयती संरक्षक की शक्तियाँ – एक वसीयत द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक को वसीयत की शर्तों की सीमा में नैसर्गिक संरक्षक को सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसे नैसर्गिक संरक्षक के सभी अधिकार तथा कर्तव्य का निर्वाह करना होगा। एक वसीयती संरक्षक का अवयस्क के भरण-पोषण का दायित्व व्यक्तिगत नहीं होता परन्तु यह दायित्व अवयस्क की सम्पत्तियों तक सीमित रहता है। परन्तु उसका यह कर्तव्य है कि अवयस्क की देखभाल तथा पोषण करें तथा यदि माता-पिता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वसीयती संरक्षक है तो वह न्यायालय से अवयस्क की देखभाल के लिए उचित धन उपलब्ध कराने की माँग कर सकता है।
लड़कियों के मामले में वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक की नियुक्ति उस लड़की के विवाह के पश्चात् समाप्त हो जाती है तथा पति उस लड़की के विवाह के पश्चात् नैसर्गिक संरक्षक का स्थान ग्रहण कर लेता है।
वसीयती संरक्षक का हटाया जाना – संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत उसकी धारा 39 के अनुसार एक वसीयती संरक्षक को न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है। संरक्षकता तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 39 उन आधारों का उल्लेख करती हैं जिनके अन्तर्गत वसीयती संरक्षक को हटाया जा सकता है। ये निम्न हैं –
(1) न्यास का या विश्वास का दुरुपयोग।
(2) अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में निरन्तर असफलता।
(3) उसके द्वारा कर्तव्य निर्वाह में अक्षम (सन्यासी या वानप्रस्थी) हो जाना।
(4) पाल्य (अवयस्क) की उचित देख-रेख करने में पाल्य या अवयस्क के साथ दुर्व्यवहार किया जाना।
((5) इस अधिनियम के प्रावधानों की निरन्तर (उपेक्षा) अवहेलना
(6) चरित्र में त्रुटि के कारण दोषसिद्धि
(7) अवयस्क जिस स्थान में रह रहा है उस स्थान के न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के बाहर जाकर वसीयती संरक्षक द्वारा निवास करना।
(8) वसीयती संरक्षक का दिवालिया या बँक्रप्ट हो जाना।
उपरोक्त आधारों के अतिरिक्त हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसीयती संरक्षक को हटाने के निम्न आधार बताये गये हैं –
(1) यदि वह हिन्दू नहीं रह गया है अर्थात् अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है।
(2) नास्तिक होने पर या सन्यासी होकर संसार छोड़ देने पर
इस प्रकार एक हिन्दू अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक पिता तथा माता होते हैं। पिता वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर है अतः माता के रहते पिता नैसर्गिक संरक्षक की हैसियत से वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है परन्तु यदि उसकी मृत्यु माता के जीवन काल में हो हो जाती है तो माता नैसर्गिक संरक्षक होने के कारण वसीयत द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है यदि वह ऐसा करती है तो उसके वसीयती संरक्षक को पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक पर वरीयता प्राप्त होगी तथा माता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक हो अवयस्क का वसीयती संरक्षक होगा। परन्तु यदि पिता ने माता के जीवन काल में हो वसीयती संरक्षक नियुक्त किया है तथा माता बिना वसीयती संरक्षक नियुक्त किये मर जातो है तो पिता द्वारा वसीयत के अन्तर्गत नियुक्त संरक्षक ही प्रभावी होगा।
एक अधर्मज सन्तान की नैसर्गिक संरक्षक उसकी माता है अतः उसे अधिकार है कि वह वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करके अपनी मृत्यु के पश्चात् पिता को अपवर्जित करके अन्य व्यक्ति को वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है।
वसीयती संरक्षक को वही अधिकार तथा दायित्व होंगे जो नैसर्गिक संरक्षक को। वसीयती संरक्षक को कतिपय आधारों पर न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है।
प्रश्न 14. (i) न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कब हो सकती है? हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसे संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के विषय में अधिकार पर क्या प्रतिबन्ध है?
When a guardian can be appointed by Court? What are the restrictions on the rights of a guardian with respect to minor’s property under Hindu Minority and Guardianship Act, 19567
(ii) निम्न में अन्तर बतायें –
(क) प्राकृतिक तथा वसीयती संरक्षक में अन्तर
(ख) वस्तुतः संरक्षक तथा विधितः संरक्षक
(a) Distinguish between Natural and Testamentary Guardian.
(b) De facto Guardian and De jure Guardian.
उत्तर (i)- भारत में संरक्षकता विधि के विकास का प्रयास स्वतन्त्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में किया गया। स्ट्रेन्ज तथा मेकनाटन के प्रसिद्ध ग्रन्थों में माता-पिता, बड़े भाई तथा अन्य न्यायालय को संयुक्त मिताक्षरा परिवार की संयुक्त सम्पत्ति में एक अवयस्क के हितों की रक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
इस स्थिति को उदाहरण से समझें– “क” एक हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित है। क अपनी विधवा तथा दो पुत्र ख तथा ग को छोड़ कर मर जाता है। ख वयस्क है तथा ग अवयस्क है। अब ख तथा ग के पास दो विकल्प है या तो वे संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रह सकते हैं या अपनी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का विभाजन करा सकते हैं। यदि ख तथा ग प्रथम विकल्प के अनुसार संयुक्त परिवर के रूप में रहना चाहते हैं तो ख तो वयस्क तथा ज्येष्ठ पुत्र है वही संयुक्त अविभाज्य सम्पत्ति के कर्ता के रूप में सम्पत्ति की व्यवस्था करेगा तथा न्यायालय को अवयस्क ग के लिए संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सम्पत्ति संयुक्त होने के कारण ग का सम्पत्ति में हित पृथक् नहीं है परन्तु यदि ग (अवयस्क) दूसरे विकल्प का चुनाव कर संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन करने की माँग करता है तथा सम्पत्ति विभाजित हो जाती है तो ग (अवयस्क) की सम्पत्ति की संरक्षकता ग की माता में निहित होगी तथा ग (अवयस्क) की माता उसकी सम्पत्ति की संरक्षक नियुक्त हो सकेगी तथा संरक्षक के रूप में अपने अवयस्क पुत्र के सम्पत्ति (विभाज्य) की व्यवस्था करेगी क्योंकि यह ग की पृथक् सम्पत्ति है।
इस विषय में दो बातें स्पष्ट हैं- (1) प्रथम तो यह कि अविभाज्य (संयुक्त) मिताक्षरा परिवार की सम्पत्ति की व्यवस्था उसका कर्ता, पिता या ज्येष्ठ सदस्य ही करेगा माता को संरक्षकता प्राप्त नहीं होगी। (2) यदि अवयस्क अपनी संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन करवाता है तो भी वह अपनी पृथक् सम्पत्ति का संरक्षक स्वयं नहीं हो सकेगा तथा उसकी माता अवयस्कता की समयावधि तक या उसके वयस्क हो जाने तथा उसकी पृथक् सम्पत्ति को संरक्षक के रूप में व्यवस्था करेगी। इस प्रकार मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में एक अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त करने का कोई अधिकार न्यायालय को नहीं है परन्तु धारा 12 के परन्तुक के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह एक वयस्क सदस्य की व्यवस्था के अधीन संयुक्त हिन्दू (मिताक्षरा तथा दायभाग) परिवार की संयुक्त सम्पत्ति में एक अवयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकती है परन्तु यह अधिकार उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय को नहीं है।
वर्तमान स्थिति – परन्तु एक हिन्दू अवयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति न्यायालयों को संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत प्राप्त है। हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 2 ने संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की वैधता को कायम (यथावत) रखा है तथा यह स्पष्ट किया है कि हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधान संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अतिरिक्त होंगे तथा इनमें विरोधाभास होने पर संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 की अवयस्क के अविभाज्य साम्पत्तिक हित के लिए संरक्षक की नियुक्ति पर न्यायालय के अधिकार पर प्रतिबन्ध होते हुए न्यायालय संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार एक हिन्दू अवयस्क को सम्पत्ति तथा शरीर के लिए संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि एक हिन्दू अवयस्क के लिए संरक्षकों के तीन वर्ग हैं –
1. प्राकृतिक संरक्षक,
2. वसीयती संरक्षक,
3. न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक
न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक – यद्यपि हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 12 एक संयुक्त मिताक्षरा परिवार की संयुक्त सम्पत्ति के निमित्त उसे परिवार के अवयस्क सदस्य के हितों के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध है फिर भी संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को एक हिन्दू अवयस्क की शारीरिक तथा साम्पत्तिक हितों की रक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति जिला न्यायालय को प्रदान की गई है। यद्यपि उच्च न्यायालय को भी यह अन्तर्निहित शक्ति प्राप्त है।
संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 एक अवयस्क की सम्पत्ति तथा शरीर के हिस्से की रक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त करने का न्यायालय को विस्तृत अधिकार देता है।
संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत जिला न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं। जब भी न्यायालय किसी अवयस्क के कल्याण के लिए किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक समझता है तो जिला न्यायालय ऐसा करने का अधिकार रखता है। न्यायालय संरक्षक नियुक्त या घोषित करने से पूर्व अवयस्क की आयु, लिंग, इच्छा और वैयक्तिक विधि, माता-पिता की इच्छा और संरक्षक की योग्यता पर ध्यान देगा (धारा 17 संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890) परन्तु संरक्षक की नियुक्ति करते समय न्यायालय के मस्तिष्क में बालक का कल्याण सर्वोपरि आधार होगा।
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत में श्रीमती स्वेता एवं अन्य बनाम धर्म चन्द एवं अन्य, ए० आई० आर० (2001) म०प्र० 23 के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। प्रस्तुत वाद में ‘अ’ जो कि एक सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति था, उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हो गयी। ‘अ’ अपने पीछे एक अवयस्क पुत्री तथा विधवा पत्नी छोड़ गया था। ‘अ’ की मृत्यु के पश्चात् अवयस्क पुत्री अपने नाना के संरक्षण में, साथ रहने लगी जो कि उसका भरण-पोषण करता था. कुछ समय पश्चात् जाना ने अवयस्क पुत्री तथा उसके अविभाज्य पैतृक सम्पत्ति में अपने को संरक्षक नियुक्त कराने के लिए एक आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना के आवेदन के साथ-साथ पुत्री के चाचा जो मृतक का सगा भाई था, उसने भी इस आशय का आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपरोक्त बाद में न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि अवयस्क पुत्री का चाचा, पुत्री के हितो को ध्यान में रखते हुये संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता तथा न्यायालय ने इस बाद में यह भी अभिनिर्धारित किया कि पुत्री के नाना उसके हितों को ध्यान में रखते हुये संरक्षक हो सकता है किन्तु अविभाज्य संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पत्ति का संरक्षक नहीं हो सकता क्योंकि यह हिन्दू अवयस्कता संरक्षक अधिनियम, 1956 की धारा 12 के विरुद्ध होगा।
हिन्दू अवयस्कता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अनुसार भी एक हिन्दू अवयस्क के संरक्षक को नियुक्ति के समय अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि आधार होगा परन्तु संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8 हिन्दू अवयस्क की संयुक्त सम्पत्ति के लिए संरक्षक से सम्बन्धित विधि को अनुमानित छोड़ती है तथा हिन्दू अवयस्क के लिए संरक्षक होने के वरीयता क्रम को यथावत रखती है। पिता एक अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक है उसके पश्चात् माता इनके अतिरिक्त कोई भी रिश्तेदार अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकता परन्तु पति अपनी अवयस्क पत्नी का संरक्षक होगा परन्तु यदि न्यायालय के विचार में पति नैसर्गिक संरक्षक होने के योग्य नहीं है तो न्यायालय अवयस्क के शारीरिक तथा साम्पत्तिक हितों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। जब न्यायालय द्वारा किसी अवयस्क को सम्पत्ति या शरीर का संरक्षक नियुक्त किया जायेगा तो नैसर्गिक संरक्षक का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।
अवयस्क की सम्पत्ति के अन्तरण पर हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध – हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 एक अवयस्क हिन्दू की सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाती है। धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसार एक संरक्षक को हिन्दू अवयस्क के कल्याण के लिए तथा उसकी सम्पत्ति के कल्याण तथा संरक्षण के लिए इस अधिनियम के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन सभी आवश्यक युक्तियुक्त तथा उचित सभी कार्य करने का अधिकार है परन्तु किसी भी परिस्थिति में एक संरक्षक अपने व्यक्तिगत प्रसंविदा द्वारा अवयस्क को बाध्य नहीं कर सकता। धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार एक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के अभाव में (1) अवयस्क की सम्पत्ति को न तो बन्धक रख सकता है न भारित कर सकता है, न ही विक्रय, दान, विनिमय या अन्यथा अवयस्क की सम्पत्ति को या उसके अंश को अन्तरित ही कर सकता है।
(2) संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति को पाँच वर्ष से अधिक समयावधि या यदि अवयस्क के वयस्क होने में एक वर्ष की अवधि शेष है तो एक वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। इस अधिनियम की धारा 8 (3) अति महत्वपूर्ण है। धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार यदि संरक्षक ने किसी हिन्दू अवयस्क की सम्पत्ति का अन्तरण इस अधिनियम को धारा 8 (2) के प्रतिबन्ध के उल्लंघन में किया है तो ऐसा अन्तरण शून्यकरणीय होगा अर्थात् धारा 8 उपधारा (4) न्यायालय को अवयस्क की सम्पत्ति के अन्तरण के लिए संरक्षक को दो जाने वाली अनुमति के विषय में है जिसके अनुसार न्यायालय ऐसी अनुमति उसी परिस्थिति में देगा जब न्यायालय के विचार में ऐसा करना अवयस्क के कल्याण के लिए अति तथा तत्काल आवश्यक है।
उत्तर (ii) (क)-प्राकृतिक तथा वसीयती संरक्षक में अन्तर (Distinction between Natural and Testamentary Guardian)
प्राकृतिक संरक्षक (Natural Guardian)
(1) प्राकृतिक संरक्षक वह व्यक्ति है जो अवयस्क से उसके सम्बन्धों के कारण संरक्षक बन जाता है। जैसे पिता-माता। सम्बन्धों में निकटता तथा रक्त सम्बन्ध सम्मिलित है।
(2) पिता अपनी अवयस्क सन्तान का स्वाभाविक संरक्षक है। अपनी अवयस्क सन्तानों पर पिता का अधिकार अनियन्त्रित है।
(3) प्राकृतिक संरक्षक अपने विवेकानुसार अपनी शक्तियों को दूसरे व्यक्ति को प्रत्यायोजित (delegate) कर सकता है।
(4) हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 प्राकृतिक संरक्षक से सम्बन्धित है।
(5) प्राकृतिक संरक्षक अवयस्क का स्वाभाविक संरक्षक है अतः अवयस्क के जन्म से ही वह कार्य करता है।
वसीयती संरक्षक (Testamentary Guardian)
(1) वसीयती संरक्षक वह है जिसे प्राकृतिक सरक्षक ने अपनी वसीयत (Will) के माध्यम से संरक्षक नियुक्त किया है।
(2) वसीयती संरक्षक की नियुक्ति का आधार वसीयत के प्रावधान हैं। अतः वसीयती संरक्षक के अवयस्क पर अधिकार वसीयत के प्रावधानों से नियन्त्रित हो सकते हैं।
(3) वसीयती संरक्षक अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता यदि ऐसा प्रावधान वसीयत के अन्तर्गत नहीं है।
(4) हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9 वसीयती संरक्षक से सम्बन्धित है।
(5) वसीयती संरक्षक प्राकृतिक संरक्षक की या वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् संरक्षक का कार्य प्रारम्भ करता है क्योंकि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावी होती है।
उत्तर (ii) (ख) – वस्तुतः संरक्षक तथा विधितः संरक्षक में अन्तर (Distinction between De facto Guardian & De jure Guardian)
वस्तुत: संरक्षक (De facto Guardian)
(1) वस्तुत: संरक्षक स्वयं नियुक्त संरक्षक होता है। इसकी नियुक्ति नहीं की जाती।
(2) वस्तुत: संरक्षक को विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
(3) वस्तुत: संरक्षक के कार्यों को साम्या के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
(4) वस्तुत: संरक्षक को अवयस्क के किसी प्रकार के हित सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं है चाहे सम्पत्ति चल हो या अचल, विभाज्य हो या अविभाज्य ।
(5) वस्तुतः संरक्षक द्वारा किया गया अन्तरण हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 के पारित होने के पश्चात् शून्य है।
विधितः संरक्षक (De jure Guardian)
(1) विधित: संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त या अन्य उचित नियम के अन्तर्गत नियुक्त संरक्षक होता है।
(2) विधित: संरक्षक को विधि तथा न्यायालय के समान मान्यता प्राप्त है।
(3) विधितः संरक्षक के कार्यों की मान्यता विधि के नियमों पर आधारित होती है।
(4) विधिक संरक्षक को अवयस्क के शरीर तथा सम्पत्ति के लाभ के लिए तथा विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत अवयस्क की सम्पत्ति का विक्रय आदि के माध्यम से हस्तान्तरण करने का अधिकार है।
(5) विधित: संरक्षक के द्वारा किया गया अन्तरण वैध है यदि वह अवयस्क के लाभ या विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत किया गया हो।
प्रश्न 15. हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आश्रितों के भरण-पोषण सम्बन्धी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में पत्नी को अलग रहने पर भी भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? क्या मुस्लिम महिला भी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है? पत्नी कब पृथक् निवास तथा भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती।
Discuss the right of maintenance of dependents under Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. When a wife can claim maintenance while living separately? Can a Muslim Women claim maintenance while living separately? When a wife cannot claim maintenance while living seperately?
उत्तर– हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा प्रथम चार ” आश्रित” शब्द प्रविष्ट हुआ। इस धारा के अन्तर्गत उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिनका भरण-पोषण मृतक के वारिसों (उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 18 से 20 तक आश्रितों को कुछ श्रेणियाँ उल्लिखित की गई हैं। धारा 18 से 20 तक उल्लिखित आश्रितों के भरण-पोषण का दायित्व सम्बन्ध (नातेदारी) के आधार पर होता है जबकि धारा 21 में उल्लिखित आश्रितों को भरण-पोषण के अधिकार सीमित दायित्वों के अधीन है। इस धारा के अन्तर्गत भरण-भोषण का आधार यह है कि जिन नातेदारों का भरण-पोषण करने हेतु मृतक उत्तरदायी था उनका भरण-पोषण करने के लिए वह व्यक्ति भी उत्तरदायी है जिसने मृतक से उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त की है।
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के निम्न नातेदार आश्रित कहलाते हैं- (1) पिता, (2) माता, (3) विधवा (4) अवयस्क धर्मज तथा अधर्मज पुत्र (5) अवयस्क अविवाहित धर्मज और अधर्मज पुत्री, (6) विधवा पुत्री, (7) विधवा पुत्रवधू (8) विधवा पौत्र वधू, (9) अविवाहित पौत्र, (10) अवयस्क प्रपौत्र (11) अवयस्क पौत्री (12) अविवाहित प्रपौत्री।
आश्रितों के भरण-पोषण के नियम- आश्रितों के भरण-पोषण सम्बन्धी निम्न नियम हैं –
(1) यहाँ अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध न होकर सम्पत्ति के विरुद्ध है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। यह दायित्व सम्पत्ति तक सीमित है। मृतक के उत्तराधिकारी से आश्रित उतना ही भरण-पोषण माँग सकते हैं जितनी कि मृतक की सम्पत्ति उसके पास है।
(2) कुछ मामलों में यह सम्भव है कि मृतक का उत्तराधिकारी तथा आश्रित एक ही व्यक्ति हो। जैसे विधवा परन्तु वास्तव में ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि इस अधिनियम की धारा 22 (2) के अनुसार आश्रित भरण-पोषण की माँग तभी कर सकता है जबकि इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् उसने मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में कोई अंश नहीं पाया है। उत्तराधिकारी चाहे वसीयती हो या अवसीयती। इस प्रकार जो व्यक्ति अधिनियम पारित होने के पश्चात् मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में अंश पाने का अधिकारी है वह आश्रित नहीं हो सकता। इस प्रकार एक पुत्र विधवा तथा पुत्री मृतक की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में अंश प्राप्त करता है अतः आश्रित के रूप में भरण-पोषण की माँग नहीं कर सकता।
(3) मृतक को सम्पत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का संयुक्त रूप से पृथक्-पृथक् दायित्व है। इस प्रकार यदि क की सम्पत्ति ग तथा घने उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा मृतक का आश्रित च है। च के भरण पोषण का ख, ग तथा घ का साथ-साथ अलग-अलग दायित्व है परन्तु यह दायित्व उनमें से प्रत्येक का दायित्व अपने द्वारा प्राप्त सम्पत्ति के अंश के अनुपात तक सीमित रहेगा। [धारा 22 (3) ]।
(4) दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 22 (4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं आश्रित है, अन्य आश्रितों के भरण-पोषण के लिए अंश देने का दायी न होगा यदि जो अंश या भाग से प्राप्त हुआ हो उसका मूल्य उससे जो उसे भरण-पोषण के रूप में इस अधिनियम के अधीन निहित हो कम हो या कम हो जायेगा यदि अभिदाय करने के दायित्व को लागू किया जाय। जैसे- एक व्यक्ति (हिन्दू) अपनी वसीयत द्वारा अपनी विधवा को कुछ सम्पत्ति देता है जिसकी वार्षिक आय एक हजार रुपया है। मृतक ने अपनी माता को भी छोड़ा है जिसे वसीयत के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति नहीं मिली है। यहाँ विधवा तथा माता दोनों आश्रित हैं। एक हजार वार्षिक की आमदनी विधवा के भरण-पोषण के लिए अपर्याप्त है। इस स्थिति में विधवा का मृतक के आश्रित का भरण-पोषण के लिए कुछ भी अंशदान करने का दायित्व नहीं है।
किन परिस्थितियों में एक पत्नी पृथक् निवास करते हुए भरण-पोषण की माँग कर सकती है- (धारा 18 (2) के अनुसार)
क्या एक हिन्दू पत्नी अपने पति से पृथक् रहते हुए अपने भरण-पोषण का दावा कर सकती है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में?
सामान्य नियम यह है कि उचित कारणों के अभाव में अपने पति की सहमति के बिना अपने पति से पृथक् रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं है। नियम का आधार यह है कि पत्नी का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने पति के अधिकार (प्रभाव) को स्वीकार कर उसकी आज्ञानुसार आचरण करे तथा उसकी (पति की) सुरक्षा में उसके साथ एक छत के नीचे रहे। परन्तु इस विधि में सुधार इसलिए आवश्यक हो गया था कि कतिपय मामलों में पत्नी, पति के अत्याचार का शिकार हो सकती थी। अतः इस नियम में संशोधन हिन्दू विवाहित स्त्री के पृथक् निवास और भरण-पोषण अधिनियम, 1946 द्वारा 1946 में किया गया। सन् 1946 में इस अधिनियम के उपबन्ध को हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। अब तक पत्नी कुछ परिस्थितियों में पृथक् निवास के साथ-साथ भरण-पं.पण का अधिकार प्राप्त कर सकती है।
सामान्य नियम के अन्तर्गत एक पत्नी अपने पति से पृथक् निवास करते हुए भरण-पोषण को अधिकारिणी नहीं है परन्तु यदि वह यह साबित करने में सफल हो जाती है कि अपने पति के गलत आचरण या किसी अन्य उचित कारण से वह अपने पति से पृथक् निवास करने के लिए बाध्य है तो वह अपने पति से पृथक् रहते हुए भी भरण-पोषण की माँग कर सकती है। हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 (62) कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसके अन्तर्गत एक पत्नी अपने पति से पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की अधिकारिणी है। ये आधार निम्न हैं –
(1) पति द्वारा त्याग या अभित्यजन- हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में अभित्यजन की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः एक पति द्वारा पत्नी का अभित्यजन कब माना जायेगा, इसका निर्णय न्यायालय की प्रत्येक वाद की परिस्थितियों के आधार पर करना होगा। अभित्यजन को गठित करने के लिए एक पत्नी को निम्न बातों को साबित करना होगा –
(1) पति ने उसका अभित्यजन किया है।
(2) पति ने उसका अभित्यजन उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा उचित कारण के अभाव में किया है।
(3) पति उसकी जान बूझकर उपेक्षा करने का दोषी है।
जब एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का अकारण ही और बिना दूसरे की सहमति के स्थायी रूप से निराकरण या परित्याग करता है तो उस क्रिया को अभित्यजन कहा जा सकता है। यह निराकरण या परित्याग का कृत्य मात्र न होकर एक आचरण है। यह एक स्थान मात्र का परित्याग नहीं बल्कि एक स्थिति का परित्याग है। इस प्रकार यदि पति घर से बाहर चला जाता है या पत्नी कुछ समय के लिए पति गृह से बाहर चली जाती है तो अभित्यजन नहीं होगा। अभित्यजन में पति का पृथक् निवास या चला जाना पत्नी से वैवाहिक सम्बन्ध के विच्छेद के आशय के साथ-साथ होना चाहिए। पंकजकी दास बनाम हृषिकेश, (1986) के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि अलगाव का तथ्य तथा मतभेद का तथ्य साथ-साथ होना चाहिए तथा अलगाव के तथ्य के साथ-साथ वैवाहिक सम्बन्धों का अन्त करने का आशय विद्यमान होना चाहिए।
(2) पति द्वारा क्रूरता (Cruelty) – क्रूरता इस प्रकार का आचरण है जिससे जीवन को, किसी शारीरिक अंग को, शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा है या खतरे की आंशका हो। मानसिक तनाव या मानसिक संत्रास के लिए परिस्थिति उत्पन्न करना भी क्रूरता की परिभाषा में आता है। क्रूरता के लिए सिर्फ एक मात्र आचरण न होकर एक से अधिक कार्य साबित करना आवश्यक है अर्थात् क्रूरतापूर्ण आचरण की बारम्बारता आवश्यक है।
क्रूरता के आधार में सिर्फ प्रहार या मारपीट ही सम्मिलित नहीं है परन्तु अपमानजनक तथा क्षोभ उत्पन्न करने वाले शब्द का बारम्ब प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का गठन करता है। इस प्रकार पति से पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की माँग क्रूरता के आधार पर करने वाली पत्नी को निम्न बातें साबित करनी होंगी- (1) यह कि पति ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण किया था। (2) यह कि क्रूरता से उसके मस्तिष्क में यह भावना उत्पन्न हुई थी कि अपने पति के साथ रहना उसके लिए नुकसानदेह या क्षतिकारक होगा।
(3) पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित हो- स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) का लोप किया गया है जिसके वजह से इस अगर को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अतः अब कुष्ठ रोग के आधार पर पृथक रहते हुए भरण-पोषण की माँग नहीं की जा सकती हैं।
(4) पति का दूसरी जीवित पत्नी के साथ निवास– हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) इस आधार पर एक पत्नी को पति से पृथक् रहते हुए भी भरण पोषण अधिनियम का अधिकार देती है कि उसका पति दूसरी जीवित पत्नी के साथ रह रहा है। परन्तु यह स्मरणीय है कि यदि दूसरी जीवित पत्नी (जिसके साथ उसका पति रह रहा है) के साथ उसके पति का विवाह शून्य विवाह है तो पत्नी इस आधार पर अपने पति से पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की माँग इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 (2) के अन्तर्गत दूसरा विवाह वैध विवाह होना चाहिए। जगदुमनी बनाम कुमुदनी, (1986) के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि पति ने अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की (अनुमति) सहमति इस आधार पर प्राप्त की है कि वह (प्रथम पत्नी) सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकी तो भी प्रथम पत्नी पति से पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की माँग कर सकती है।
यह उल्लेखनीय है कि चूँकि इस अधिनियम का आशय द्विपत्नी विवाह से हतोत्साहित करना है अतः यदि पति ने दूसरा विवाह अधिनियम के पारित होने के पूर्व भी किया है तो भी पत्नी को पृथक् रहते हुए भरण-पोषण की माँग करने का अधिकार होगा यदि दूसरा विवाह अधिनियम के पारित होने के पश्चात् तक जारी रहता है।
(5) पति ने रखैल रख ली हो– इस आधार के अन्तर्गत एक पत्नी को अपने पति से पृथक् रहते हुए भी भरण-पोषण की माँग का अधिकार प्राप्त करने के लिए दो बातें साबित करनी होंगी- (1) यह कि उसका पति रखैल रखता है। (2) वह रखैल उसी घर में रहती है जिस घर में पत्नी भी रहती है या प्रति आदतन अपनी रखैल के साथ पृथक् निवास में रहता है।
नरेन्द्र अप्पा भाटकर बनाम निलम्मा, ए० आई० आर० (2013) एस० सी० 1541 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए निर्णय किया कि जहाँ कोई पत्नी अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो और जहाँ न्यायालय आपसी सुलह समझौता के आधार पर बाद को निस्तारित कर दिया हो, और पति-पत्नी के बीच स्थायी रूप से अलगाव भी हो चुका हो, वहाँ पत्नी को हिन्दू भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का उसका अधिकार समाप्त नहीं माना जायेगा बल्कि पत्नी इस अधिनियम के अन्तर्गत भरण-पोषण की माँग कर सकती है।
श्रीमती कल्पना पण्डित बनाम किसहो पण्डित, ए० आई० आई० आर० (2016) कलकत्ता के बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के अन्तर्गत पत्नी को भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाहित है, यदि पत्नी अलग रहने का उचित कारण स्पष्ट कर देती है, वहाँ पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिये बाध्य होगा।
क्या मुस्लिम महिला भी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है?
हाँ, विवाह के दौरान एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए पूर्ण दायित्व के अधीन है, पति का अपनी पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व पत्नी के यौवनागमन के प्रारम्भ से ही प्रारम्भ होता है, उसके पूर्व नहीं।
तलाक (विवाह-विच्छेद) के पश्चात् मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक तलाक शुदा महिला को अपने पति से सिर्फ इद्दत काल के दौरान ही भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है।
मुस्लिम विधि में पति द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने की दशा में पत्नी पृथक रहकर भी भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है बशर्ते भरण-पोषण प्राप्त करने का करार न तो अवैध हो और न ही लोकनीति के प्रतिकूल पत्नी कब पृथक् निवास तथा भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती – निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी को पृथक् निवास तथा भरण-पोषण का अधिकार नहीं रह जाता –
(1) जब वह धर्म परिवर्तन करके हिन्दू नहीं रह जाती।
(2) जब वह असाध्वी हो जाती है।
(3) जब वह किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना पृथक् निवास करती है।
(4) जब पति-पत्नी में आपसी समझौते के परिणामस्वरूप पत्नी अलग रहती है और अपने भरण-पोषण का दावा त्याग देती है।
गुन्टा मुकाला बनाम गुन्टा मुकाला सुधाकर व अन्य, ए० आई० आर० (2013) आन्ध्र प्रदेश 58 के मामले में उच्च न्यायालय ने अभिकथन दिया कि जब पत्नी का आचरण अपने पति के प्रति अनादरपूर्ण हो और पति ने पत्नी के इस आचरण से शुब्ध होकर उसका अभिल्याग कर दिया हो तो पत्नी अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं रह जायेगी।
प्रश्न 16 पत्नी, विधवा-पुत्रवधू, बालक और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण के अधिकारों की विवेचना कीजिए?
Discuss the right of maintenance of wife, widowed daughter in-law, children and aged parents.
उत्तर – हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्नी, विधवा पुत्र-वधू, बच्चे तथा वृद्ध माता-पिता को भरण पोषण सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है –
1. पत्नी- अधिनियम की धारा 18 के अधीन दो प्रकार के अधिकार दिये गये हैं –
(i) भरण-पोषण
(ii) पृथक् निवास का अधिकार
इस अधिनियम के पूर्व भी हिन्दू विवाहिता स्त्रियों के पृथक् निवास का अधिकार तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1946 लागू था जो अब हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पत्नी को भरण-पोषण का निम्न अधिकार प्राप्त है –
1. हिन्दू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरम्भ के पूर्व या बाद व्याही गई हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण-पोषण पाने के लिए हकदार, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगी।
बरूम्मा बनाम सिधप्पा जीवाप्पा, ए० आई० आर० 2003 कर्नाटक 243 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि भरण-पोषण के अधिकार को विवाह-विच्छेद के करार के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता तथा कोई भी भरण-पोषण के अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से नहीं प्रदत्त किया जायेगा।
रघुवीर सिंह बनाम गुलाब सिंह, ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 240 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि पत्नी का भरण-पोषण अधिकार का जन्म सामाजिक एवं सांसारिक बन्धन के परिणामस्वरूप हुआ। पत्नी के अन्तर्गत तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है। चाँद धवन बनाम जवाहर लाल धवन, 3 एस० सी० सी० 1993 पृ० 406 के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार यदि पति की कोई दायर याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 से धारा 14 के अन्तर्गत खारिज हो जाती है तो हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत पत्नी भरण-पोषण का दावा कर सकती है, किन्तु न्यायालय धारा 18 (1) के अन्तर्गत भरण-पोषण का सामान्य अनुतोष हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 में कार्यवाहियों में नहीं प्रदान कर सकता ।
(2) हिन्दू पत्नी भरण-पोषण के अपने दावे को खोये बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए उस सूरत में हकदार होगी जिसमें कि-
(क) उसका पति अभित्यजन का, अर्थात युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या कामतः उसकी उपेक्षा करने का दोषी है।
(ख) उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार कर चुका है जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो गया है कि मेरे लिये अपने पति के साथ रहना क्षतिकारक होगा,
(ग) उसका पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वर्तमान में स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा इस आधार का लोप कर दिया गया है जब उग्र कुष्ठ रोग पृथक रहने का आधार नहीं हो सकता।]
(घ) उसके पति की अन्य कोई पत्नी जीवित हो,
(ङ) उसका पति उसी मकान में, जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में निवास करता है,
(च) उसका पति कोई अन्य धर्म ग्रहण करने के कारण हिन्दू नहीं रहा है, और
(छ) उसके पृथक् होकर रहने को न्यायानुमत करने का कोई अन्य कारण हो।
(3) यदि कोई हिन्दू पत्नी असली है या किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने के कारण हिन्दू नहीं रहती है और पृथक् निवास करती है तो वह भरण-पोषण की अधिकारी नहीं होगी।
विधवा पुत्र-वधू का भरण-पोषण– (1) कोई हिन्दू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व या बाद में विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने श्वसुर द्वारा भरण-पोषण के लिए हकदार होगी, (धारा 19)
परन्तु यह तब जब कि उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है या, जहाँ कि उसके पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति नहीं है, वह –
(क) अपने पति या अपने पिता या माता की सम्पदा से, या
(ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, या उसकी सम्पदा से भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ है।
बलवीर कौर बनाम हरिन्दर कौर, ए० आई० आर० 2003 पंजाब 174 के बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के अन्तर्गत अपने श्वसुर के विरुद्ध विधवा बहू द्वारा भरण-पोषण के दावे का अधिकार श्वसुर के पास उपलब्ध सहदायिको सम्पत्ति की सीमा तक सीमित है, जिसमें विधवा बहू ने किसी अंश को नहीं लिया।
2. यदि श्वसुर के अपने कब्जे में किसी समांशित सम्पत्ति से जिसमें से पुत्र-वधू को कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ है, श्वसुर के लिए करना साध्य नहीं है, तो उपधारा (1) के अधीन किसी आभार का अनुपालन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसा कोई आभार पुत्र-वधू के वाह पर न रहेगा।
बालकों और वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण – 1. इस धारा (20) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई हिन्दू अपने जीवन काल के अभ्यन्तर अपने औरस या जारज बालकों और वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है।
2. जब तक कि औरस या जारज बालक अवयस्क रहे, वह अपने माता या पिता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा।
3. अपने वृद्ध माता पिता या दुर्बल बालकों का या किसी पुत्री का, जो कि अविवाहित हो, भरण-पोषण करने से किसी व्यक्ति के आभार का विस्तार वहाँ तक होगा जब तक कि जनक या अविवाहित पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।
आनन्दी डी जाधव बनाम निर्मल चन्द्र कौर, ए० आई० आर० 2000 एस० सी० 1386 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जहाँ माता-पिता अत्यन्त दयनीय दशा में हों, तो उनका भरण-पोषण उनके पुत्रों द्वारा किया जायेगा।
एस० जगजीत सिंह भाटिया बनाम बलबीर सिंह भाटिया, ए० आई० आर० 2003 एन० ओ० सी० 450 के बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण करना पुत्र का व्यक्तिगत दायित्व है चाहे उसने अपने पिता की सम्पत्ति दाय में प्राप्त किया हो या न किया हो।
विश्वम्भर बनाम धान्या व अन्य, ए० आई० आर० (2005) केरल 91 के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने दत्तक ग्रहण भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियों के सम्बन्ध में एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने वैध अथवा अवैध सन्तानों के भरण-पोषण के साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया कि पुत्री अपने माता-पिता से भरण-पोषण वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात् भी ले सकती है जब तक कि पुत्री का विवाह न हुआ हो अथवा वह स्वयं जीविकोपार्जन न कर रही हो।
पुनः नलिनी श्यामल व अन्य बनाम वृद्धावन श्यामल, ए० आई० आर० (2014) (NOC) 444 उड़ीसा के बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पुत्री के भरण-पोषण के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ पति ने अपनी किसी अवैध सन्तान को वैध रूप से स्वीकार कर लिया हो वहाँ ऐसी सन्तान अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी।
प्रश्न 17. (i) संयुक्त हिन्दू परिवार की संरचना कीजिए। (उद्गम) एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए।
Explain the Nature and origin of Joint Hindu Family.
(ii) हिन्दू सहदायिकी से आप क्या समझते हैं? सहदायिकी के प्रमुख लक्षण या विशेषतायें बतलाइये तथा संयुक्त हिन्दू परिवार से इसका अन्तर स्पष्ट कीजिए।
What do you understand by Hindu Coparcenary? Explain the characteristics of coparcenary and distinguish it from a Joint Hindu Family.
(iiii) सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायिकों के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।
Explain the rights of coparceners over coparcenary property.
उत्तर- (i) संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकृति – संयुक्त परिवार हिन्दुओं की एक अति प्राचीन संस्था है। प्राचीन काल में हिन्दू एक संयुक्त परिवार में रहने के अभ्यस्त थे। इस परिवार में ऐसे सभी व्यक्ति आते हैं जिनसे परिवार निर्मित होता है। इस तरह एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति तथा उनकी पत्नियाँ एवं अविवाहिता पुत्रियाँ संयुक्त परिवार को सदस्या मानी जाती है। विवाहिता पुत्रियाँ अपने पिता के परिवार की सदस्या नहीं होती हैं। सामान्यतया हिन्दू परिवार संयुक्त होता है, न केवल सम्पदा के सम्बन्ध में वरन् उपासना तथा भोजन के सम्बन्ध में भी।
मिताक्षरा विधि में सम्पत्ति का होना संयुक्त परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं है। किन्तु जहाँ लोग संयुक्त रूप में रहते हैं तथा संयुक्त रूप से भोजन एवं उपासना करते हैं वहाँ यह धारणा युक्तियुक्त नहीं लगती कि उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। परिवार की समस्त सम्पत्ति को संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त हिन्दू परिवार उन सभी पुरुष सदस्यों से जो एक समान पूर्वज को सन्तान हैं तथा उनको माता, पत्नी अथवा विधवा तथा अविवाहिता पुत्रियों से निर्मित होता है, यह सपिण्डता के मूल सिद्धान्त पर आधारित होता है।
एक पूर्वज का होना संयुक्त परिवार के प्रारम्भ के लिए आवश्यक है, उसके चालू रहने के लिए नहीं अर्थात् पूर्वज की मृत्यु के पश्चात् भी संयुक्त परिवार चलता रहता है। अधमंज पुत्र यद्यपि सहदायिक नहीं है परन्तु अपने पिता के संयुक्त परिवार का सदस्य है। संयुक्त हिन्दू परिवार निगम नहीं होता। इसका कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं है यह अपने सदस्यों को छोड़कर अपने आप में एक पृथक् सत्ता नहीं हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार एक इकाई है जो अपना समस्त कार्य- व्यापार अपने कर्त्ता द्वारा करती है। आयकर आयुक्त बनाम सुरजीत सिंह, ए० आई० आर० (1976) एस० सी० 109 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि संयुक्त हिन्दू परिवार के लिए यह जरूरी है कि उसमें कम से कम दो व्यक्ति हों। एक अविवाहित पुरुष हिन्दू संयुक्त परिवार की स्थापना नहीं कर सकता।
संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरुष सदस्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं –
(1) वे पुरुष जो पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं;
(2) साम्पार्रिवक
(3) दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित,
(4) दीन आश्रित तथा
(5) यह उन पुत्रों को भी सम्मिलित करता है जो विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत एक हिन्दू पुरुष तथा ईसाई माता से उत्पन्न हुए हैं।
जबकि स्त्री सदस्यों में सम्मिलित है –
(1) पुरुष सदस्यों की पत्नी एवं विधवा पत्नी; तथा
(2) उसको कुमारी पुत्रियाँ।
कभी-कभी विधवा पुत्रियाँ, जो पिता के परिवार में आकर रहने लगती हैं, संयुक्त परिवार की सदस्या मान ली जाती हैं और उन्हें भरण-पोषण का हक उत्पन्न हो जाता है।
सामान्यतया प्रत्येक संयुक्त परिवार खान-पान, पूजा अर्चना और सम्पत्ति में संयुक्त होता है, परन्तु यदि वह इनमें से किसी एक या तीनों में ही संयुक्त न हो तो इसमें यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संयुक्त कुटुम्ब संयुक्त नहीं रहा है।
यह विभक्त होने का सबूत हो सकता है परन्तु निष्कर्षीय सबूत नहीं। जैसे संयुक्त सम्पत्ति के स्वामी तीन भाई पृथक्-पृथक् स्थानों में कार्यरत होने के कारण उनका संयुक्त कुटुम्ब समाप्त नहीं हो सकता है।
संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति का विक्रय विधि आवश्यकता के बिना तथा सहदायिकियों की सम्पत्ति के बिना नहीं किया जा सकता। [शारदा (मृतक) बनाम मनोहर एवं अन्य, (2004)]
उत्तर- (ii) सहदायिकी संयुक्त हिन्दू परिवार से संकुचित तथा पृथक् निकाय है। एक संयुक्त परिवार के अन्तिम पुरुष सदस्य की तीन पीढ़ी तक सहदायिकी में सम्मिलित है। उसमें वह पुरुष सहदायिक भी सम्मिलित है जिससे तीन पीढ़ी तक की गिनती की जाती है। इस प्रकार एक सहदायिकी में पिता, पुत्र, पुत्र का पुत्र अर्थात् पौत्र तथा पुत्र के पुत्र का पुत्र प्रपौत्र सम्मिलित हैं। सहदायिक (Coparcener) उन पुरुष सदस्यों को कहते हैं जो संयुक्त हिन्दू परिवार में अंश प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं-पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र
संयुक्त सम्पत्ति के धारक के सम्बन्ध में नरेन्द्र बनाम वेल्थ टैक्स कमिश्नर, ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 14 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सहदायिकी एक लघु निकाय है तथा उसमें सिर्फ तीन पीढ़ी के पुरुष वंशज (Descendants) सम्मिलित के होते हैं जिन्हें संयुक्त हिन्दू सहदायिकी सम्पत्ति में जन्म से हित प्राप्त होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार सहदायिकी में अन्तिम सम्पत्ति धारक (Last Property Holder) से तात्पर्य है लाइन का सबसे ज्येष्ठ जीवित पूर्वज (Last surviving descendant)
क – ख – ग – घ – ङ – च – छ – ज
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
उपरोक्त आरेख में ‘क’ प्रारम्भिक पूर्वज है तथा ‘ख’ से ‘ज’ तक एक लाइन से सात वंशज है। ‘क’ के जीवन काल में ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ सहदायिकी (Coparcenary) के सदस्य हैं। ‘क’ के पश्चात् तीन पीढ़ी तक के सदस्य सहदायिकी के सदस्य माने जाते हैं। ‘क’ पिता, ‘ख’ पुत्र, ‘ग’ पौत्र तथा ‘घ’ प्रपौत्र हैं। यही सहदायिकी का गठन करते हैं। ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’ तथा ‘ज’ सहदायिकी के सदस्य नहीं हैं। ‘क’ की मृत्यु पर सहदायिकी ‘ख’ से प्रारम्भ होकर ङ तक तीन पीढ़ी तक जायेगी। ‘क’ की मृत्यु के पश्चात् ङ भी सहदायिकी में सम्मिलित हो जाता है क्योंकि ‘क’ की मृत्यु के पश्चात् ‘ख’ सहदायिकी सम्पत्ति का अन्तिम धारक बन जाता है। ‘ख’ को छोड़कर सहदायिकी तीन पीढ़ी तक विस्तृत होगी तथा ‘ख’ को सम्मिलित कर अर्थात् सहदायिकी के अन्तिम धारक को सम्मिलित कर चार पीढ़ी सहदायिकी का निर्माण करती है। इसके नीचे के सदस्य सहदायिकी का निर्माण नहीं करते। इसी प्रकार यदि ‘ख’ की मृत्यु हो जाती है तो सहदायिकी ‘ग’ से प्रारम्भ होकर ‘च’ तक चार पीढ़ियों तक विस्तृत करेगी। अन्तिम धारका को छोड़कर सहदायिकी नीचे की तीन पीढ़ियों तक विस्तृत होगी, उसके पश्चात् के सदस्य सहदायिकी के अन्तर्गत नहीं आते। इसी प्रकार सहदायिकी निरन्तर रहती है और सहदायिकी के ऊपर वाली पीढ़ी के अन्तिम धारक की मृत्यु पर नीचे के सदस्य सहदायिकी के अन्तर्गत सम्मिलित होते जाते हैं। किसी भी सदस्य की मृत्यु से सहदायिकों का विघटन (Dissolution) नहीं होता, जबकि भागीदारी फर्म में यदि फर्म के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का विघटन हो जाता है।
यह स्मरणीय है कि सहदायिकी कहाँ तक विस्तृत होगी इसका निर्धारण इस आधार पर होगा कि सहदायिकी का अन्तिम धारक कौन है। अन्तिम धारक के जीवित रहते उसके नीचे की पीढ़ों के सदस्य की मृत्यु होने पर सहदायिकी नीचे की पीढ़ी तक विस्तृत नहीं होती परन्तु सहदायिकी के सदस्यों की संख्या घट जाती है। जैसे- क ख ग घ ङ च छ ज की लाइन में यदि ‘क’ अन्तिम धारक जीवित रहता है तथा ‘ख’ की मृत्यु हो जाती है तो सहदायिकी ‘घ’ से नीचे नहीं जायेगी परन्तु ‘ख’ की मृत्यु पर सहदायिकी में ‘क’, ‘ग’, ‘घ’ ही सम्मिलित होंगे तथा सहदायिकी के सदस्यों की संख्या घट जायेगी।
क – ख की मृत्यु – ग – घ – ङ – च – छ – ज
| |
सहदायिकी ‘क’ से ‘घ’ तक
यही स्थिति ‘क’ के जीवन काल में ‘ग’ या ‘घ’ की मृत्यु से होगी।
यदि उपरोक्त आरेख में ‘क’ के जीवन काल में ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ की मृत्यु हो जाती है तो ‘क’ एकमात्र सहदायिकी (Sole Surviving Coparcenar) बच जायेगा तथा सहदायिकी का अस्तित्व संकटपूर्ण हो जाता है। ‘ख’, ‘ग’ तथा ‘घ’ के मरने पर ‘क’ एकमात्र (सम्पत्ति धारक पूर्वज) सहदायिकी रह जायेगा। ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’ अब भी उससे चार डिग्री से अधिक दूर हैं। अतः सहदायिकी समाप्त हो जायेगी। यदि ‘क’ मर जाता है तथा साथ-साथ ‘ख’ ‘ग’ भी मर जाते हैं तो सहदायिकी ‘घ’ से प्रारम्भ होगी तथा ‘घ’ से चार पीढ़ी ‘ङ’, ‘च’ तथा ‘छ’ तक विस्तृत होगी।
सहदायिकी को अग्रलिखित उदाहरण से समझें –
A (अन्तिम धारक)
| चार पुत्र
———————————————————-
| | | |
B C D E
| | |
B1 S1 S2 M S
B2 N1
B3 N2
B4 N3
यहाँ B, C, D, E पुत्र B1, SI, S2. M. S पौत्र तथा B2, NI सहदायिकी होंगे परन्तु ऊपरी निचली पीढ़ी के पुरुष सहदायिक नहीं होंगे। इसे सहदायिकी में सहदायिकी कहा जाता है।
सहदायिकों का अन्तिम धारक के पश्चात् तीन पीढ़ियों तक विस्तृत होने के पीछे कारण यह है कि हिन्दुओं में तीन पीढ़ियों तक ही पुरुष वंशज अपने पूर्वजों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाने के लिए सक्षम है। महिलाओं को सहदायिकों से अपवर्जित किया गया है। इसका कारण यह है कि महिलाओं को संयुक्त हिन्दू सम्पत्ति में विभाजन का दावा करने का अधिकार नहीं है तथा सहदायिकी वही व्यक्ति है जिसे संयुक्त हिन्दू सम्पत्ति में विभाजन का दावा करने का अधिकार है। यह स्मरणीय है कि यद्यपि महिलाओं को संयुक्त हिन्दू सम्पत्ति में विभाजन का दावा करने का अधिकार नहीं है परन्तु माता तथा विधवा ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में विभाजन हो जाने के पश्चात् अपना अंश (Share) माँगने का अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा सहदायिक सम्पत्ति में पुत्रियों को भी पुत्र के समान पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा दे दिया गया है।
मिताक्षरा सहदायिकी के आवश्यक लक्षण (Essential elements of Mitakshara Coparcenary) – हितों की निरन्तरता तथा सहदायिकों के सभी सदस्यों के मध्य कब्जे की एकात्मकता मिताक्षरा सहदायिकी का विशिष्ट लक्षण है। सहदायिकी को संयुक्त कब्जे तथा संयुक्त सम्पत्ति के एकीकृत उपभोग का अधिकार है। संयुक्त स्वामित्व या स्वामित्व की एकात्मकता मिताक्षरा सहदायिकी की आवश्यक शर्त है जब तक संयुक्त हिन्दू परिवार में विभाजन नहीं हो जाता, परिवार का कोई भी सदस्य यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि संयुक्त हिन्दू परिवार में उसका अंश क्या है? सहदायिकी का सृजन जन्मत: है। सहदायिको करार (अनुबन्ध) या संविदा से सृजित नहीं की जा सकती। इस प्रकार मिताक्षरा सहदायिकी विधि द्वारा सृजित होती है करार (अनुबन्ध) द्वारा नहीं। परन्तु जहाँ एक पुत्र दत्तक के रूप में लिया गया है, निःसन्देह दत्तक पुत्र सहदायिकी में निहित (न्यागत : devolve) हो जाता है। [स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम घमण्डी लाल, ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 1330.]
मिताक्षरा सहदायिकी के आनुषंगिक (Incidental) प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं –
(1) अन्तिम धारक या समान पूर्वज से तीन पीढ़ी तक पुरुष वंशज सहदायिकी का निर्माण करते हैं;
(2) सिर्फ सहदायिकी के सदस्य हो संयुक्त परिवार सम्पत्ति में विभाजन की माँग कर सकते हैं।
((3) जब तक संयुक्त सम्पत्ति में विभाजन प्रभावी नहीं हो जाता तब तक परिवार की संयुक्त सम्पत्ति में प्रत्येक सहदायिकी का अविभाज्य समान नियन्त्रण होता है;
(4) सहदायिकी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (विक्रय, बन्धक) सिर्फ आवश्यकता के अन्तर्गत होता है, वह भी अन्य सहदायिकियों की सहमति से;
(5) सहदायिकी सम्पत्ति का स्वामित्व तथा कब्जे का अधिकार संयुक्त होता है;
(6) किसी भी सहदायिकी की मृत्यु पर उसका अंश उत्तराधिकार से नहीं परन्तु उत्तरजीविता (Survivorship) से दूसरे सहदायिकियों पर चला जाता है।
सहदायिकी का अन्त (End of Coparcenary)- सहदायिकी का अन्त दो प्रकार से होता है
(1) विभाजन से; तथा
(2) अन्तिम उत्तरजीवी सहदायिक की मृत्यु से।
मिताक्षरा सहदायिकी के प्रमुख लक्षण (Characteristics of Mitakshara Coparcenary)- मिताक्षरा सहदायिकी के प्रमुख लक्षण निम्न हैं –
(1) स्वामित्व की एकात्मकता (Unity of Ownership); (2) अंश को अनिश्चितता या अपरिनिर्धारिता (Indeterminability of Shares)
(3) हितों की सामुदायिकता (Community of Interest);
(4) महिलाओं की अपवर्जितता (Exclusion of Females);
(5) भरण-पोषण का अधिकार (Right of Maintenance); तथा
(6) उत्तरजीवितता की न्यागतता (devolution) निहित होना।
(1) स्वामित्व का ऐक्य (एकात्मकता) (Unity of Ownership)– मिताक्षरा सहदायिकी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यहाँ परिवार की सम्पत्ति पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता। परिवार की सम्पत्ति पर सभी सहदायिकों का संयुक्त स्वामित्व होता है। यहाँ स्वामित्व का ऐक्य (Unity) होता है। सम्पत्ति का स्वामित्व सम्पूर्ण सहादायिकी निकाय में निहित होता है। जब तक विभाजन प्रभावी नहीं होता, कोई भी सदस्य अपने अंशों को निर्धारित या निश्चित नहीं कर सकता। सहदायिकों का अंश एक सहदायिकों के जन्म पर घटता है तथा मृत्यु पर बढ़ता है सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायिक जन्म से अपने पिता के समान अंश प्राप्त कर लेता है। (थम्मा वेंकट सुबम्मा बनाम थम्मा रसम्मा, ए० आई० आर० 1987 एस० सी० 1775 ) ।
(2) अंश की अपरिनिर्धारितता (Indeterminability of Share) या दोलायमान हित (Fluctuating Interest) – सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायिकों का हित स्थिर या निश्चित न होकर चलायमान (दोलायमान : Fluctuating) अथवा अपरिनिर्धारित (अनिश्चित) होता है। परिवार में किसी सहदायिकी के जन्म से सहदायिकों का हित घट जाता है तथा सहदायिकों की मृत्यु पर प्रत्येक सहदायिक के हित में वृद्धि होती है। जब तक संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में विभाजन प्रभावित नहीं होता, कोई भी सहदायिक व्यक्तिगत रूप से यह घोषित नहीं कर सकता कि सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित क्या है। दानकर आयुक्त बनाम एम० एस० गेट्टी चेट्टियार, ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 410 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक परिवार अविभाजित रहता है, तब तक कोई भी सहदायिक, सहदायिकी सम्पत्ति में किसी विशिष्ट हित का अधिकारी (हकदार) नहीं है। सभी सहदायिक सम्पूर्ण सम्पत्ति के स्वामी होते हैं। उनका हित विभाजन पर ही (निश्चित) निर्धारित होता है।
(3) हितों की सामुदायिकता (Community of Interests) या हितों की ऐक्यता (Unity of Interest)— मिताक्षरा सहदायिकी का संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में सामूहिक स्वामित्व (Community Ownership) होता है। कोई भी सहदायिक पृथक् या एकाकी रूप से यह नहीं कह सकता कि “यह सम्पत्ति या अमुक सम्पत्ति मेरी है।” सहदायिक सिर्फ यह कह सकते हैं कि यह सम्पत्ति हमारी (हम सबकी) है। प्रत्येक सहदायिक जन्म के साथ उस समुदाय का सदस्य बन जाता है। जब तक वह जीवित है, उसे सम्पत्ति के उपभोग तथा प्रयोग का अधिकार होता है। उसके मृत होने पर संयुक्त सम्पत्ति में उसका हित उत्तरजीविता (Survivorship) से अन्य सहदायिकों पर चला जाता है। यहाँ पिता था अन्तिम हितधारक को किसी सहदायिक का हित छीनने का अधिकार नहीं होता क्योंकि प्रत्येक सहदायिक जन्म से ही संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपरिनिर्धारित हित प्राप्त कर लेता है जो विभाजन पर ही निश्चित होता है। विभाजन से पूर्व यह हित संयुक्त तथा चलायमान (दोलायमान Fluctuating) होता है तथा संयुक्त सहदायिकी परिवार के किसी सहदायिक के जन्म से घटता है तथा किसी सहदायिक की मृत्यु से किसी अन्य सहदायिक के हित में वृद्धि होती है।
(4) महिलाओं का सहदायिकी से अपवर्जन (Exclusion of female from Coparcenary)- मिताक्षरा सहदायिकी में किसी महिला को सहदायिकी का सदस्य होने की अनुमति नहीं यद्यपि महिलाएँ संयुक्त परिवार की सदस्य हैं। यहाँ तक कि पत्नी को सिर्फ भरण-पोषण का अधिकार है। परन्तु वे सहदायिक (Coparcener) कभी नहीं हो सकतीं। पुत्रा बीवी बनाम राजा किसन दास, (1904) 31 कलकत्ता 476. इस प्रकार महिला को सहदायिकी की संयुक्त सम्पत्ति में विभाजन की माँग करने का अधिकार नहीं है। एक महिला संयुक्त सहदायिकी परिवार की कर्ता नहीं हो सकती। एक महिला द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का हस्तान्तरण उसके पुत्रों तथा पुत्रियों पर बाध्यकारी नहीं होगा। उसके अपने अंशों का अन्तरण भी इस पर बाध्यकारी नहीं है।
यह उल्लेखनीय है कि हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 विधवा को विशेष स्थिति (Special Status) प्रदान करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वह अपने पुत्रों के साथ सहदायिकी हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करती हैं। भले ही उसने इस अंश को सीमित परिसम्पत्ति के रूप में प्राप्त किया है। एक महिला सहदायिकी सम्पत्ति में अंश सीमित परिसम्पत्ति के रूप में प्राप्त करती है परन्तु एक बार अंश प्राप्त कर लेने पर वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने पुत्र की भाँति अंश प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए ‘अ’ अपने दो पुत्र ‘ब’ तथा ‘स’ एवं विधवा ‘क’ को छोड़कर मर जाता है। अब हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार (Hindu Womens Right to Property Act, 1937) का प्रभाव यह है कि विधवा ‘क’ को ‘अ’ की सम्पत्ति में अपने पुत्रों ‘ब’ तथा ‘स’ के समान ही 1/3 अंश (भाग) प्राप्त होगा।
(5) उत्तरजीविता का न्यागमन (निहित) होना (Devolution of Survivor ship) – सहदायिकी का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि सहदायिकी सम्पत्ति में सहदायिकी हित, सहदायिक (Coparcener) की मृत्यु पर उसके वंशजों या उत्तराधिकारियों पर उत्तराधिकार के द्वारा न्यागमित (devolve) नहीं होता परन्तु यह उत्तरजीविता के रूप में अन्य सहदायिकों पर न्यागमित (devolve) होता है। उत्तराधिकार में उत्तराधिकारी को सम्पत्ति में हक (अधिकार) या स्वामित्व सम्पत्तिधारी की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हो जाता है परन्तु उत्तरजीविता (Survivorship) के अन्तर्गत किसी सहदायिक (Coparcener) को सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व जन्म से या गर्भ में आने पर ही प्राप्त हो जाता है। वह संयुक्त सम्पत्ति में जन्म से ही संयुक्त स्वामित्व प्राप्त कर लेता है परन्तु उसका हित या स्वामित्व बँटवारे के पूर्व अनिश्चित रहता है जो बँटवारे के पश्चात् निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यहाँ कब्जा भी पृथक् न होकर सभी सहदायिकों का संयुक्त रूप से होता है।
(6) भरण-पोषण का अधिकार (Right of Maintenance)- सहदायिकी के सभी सदस्यों को जन्म से हो सहदायिकी को संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार निरन्तर रहता है। जहाँ किसी सदस्य को सहदायिको सम्पत्ति में अंश नहीं मिलता वहाँ विभाजन के पश्चात् उसे भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें विभाजन में अंश प्राप्त नहीं हुआ है, विभाजन के समय कुछ प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अविवाहिता लड़कियाँ, मूर्ख व्यक्ति या पागल व्यक्ति, महिला सदस्यों को विभाजन के समय संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में अंश प्राप्त नहीं होता। अविवाहिता लड़कियों को संयुक्त परिवार सम्पत्ति से विवाह का खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पुत्री को चाहे वह विवाहिता हो अथवा अविवाहिता हो, उसको मिताक्षरा सहदायिको सम्पत्ति के अन्तर्गत जन्म से अधिकार दे दिया गया है। वह विभाजन में पुत्रों के साथ समान भागिता के अन्तर्गत सम्पत्ति धारण करेगी।
यदि कोई सहदायिक (Coparcener) विशिष्ट विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात् पृथक् सहदायिकी का निर्माण करता है।
संयुक्त हिन्दू परिवार तथा सहदायिकी में अन्तर (Distinction between Joint Hindu Family and Coparcenary) – संयुक्त हिन्दू परिवार एवं सहदायिकी में निम्नलिखित भिन्नतायें हैं –
(1) संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती, जबकि सहदायिकी संयुक्त परिवार के केवल कुछ निश्चित सदस्यों के लिए होती है।
(2) सहदायिकी केवल उन पुरुष सदस्यों तक ही सीमित होती है जो पूर्वज से उसको सम्मिलित करके, चार पीढ़ी के अन्तर्गत आते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में इस प्रकार की कोई भी सीमिततायें नहीं रहतीं।
(3) सहदायिकी केवल पुरुष सदस्यों तक ही सीमित होने के कारण अन्तिम सहदायिकी की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि संयुक्त परिवार ऐसे सहदायिक की मृत्यु के बाद भी स्थिर रहता है।
(4) प्रत्येक सहदायिकी या तो संयुक्त परिवार होता है या उसका भाग, किन्तु इसके विपरीत प्रत्येक संयुक्त परिवार सहदायिकी नहीं है।
उत्तर-(iii) सहदायिकी सम्पत्ति पर सहदायिकों के अधिकार (Rights of coparceners over coparcenary property)– सहदायिकों के अधिकार निम्नलिखित हैं –
(1) संयुक्त कब्जे तथा संयुक्त उपभोग का अधिकार (Right to joint possession and joint enjoyment)– जब तक संयुक्त परिवार सम्पत्ति में विभाजन प्रभावी नहीं होता, किसी भी सहदायिक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह सम्पत्ति मेरी है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर उनका संयुक्त कब्जा होता है। कामता नाचियार बनाम राज्य ऑफ शिवगंगा, (1863) 9 एम० आई० ए० 543 नामक वाद में प्रियो काउन्सिल ने कहा-संयुक्त परिवार सम्पत्ति में किसी भी सहदायिकी को आत्यन्तिक कब्जे (Exclusive Possession) का अधिकार नहीं होता। परिवार के सभी सदस्यों के मध्य सामुदायिक हित तथा कब्जे की एक्यता रहती है। उनमें से किसी की मृत्यु पर अन्य सदस्य उत्तरजीविता के द्वारा वह सभी पा जाते हैं जो मृतक के जीवन काल में सामान्य हित तथा सामान्य कब्जे के अन्तर्गत था।
एक बाद में एक संयुक्त परिवार में एक सहदायिकी को सीढ़ी (जीना: Staircase) तथा दरवाजे का प्रयोग करने से रोका गया जिससे उस कमरे में जाया जाता था, जो उसके कब्जे में था, बम्बई उच्च न्यायालय ने (अनन्त बनाम गोपाल, 11 बम्बई 269) उसके विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया।
(2) संयुक्त या सामुदायिक हित का अधिकार (Right of Community Interest)– संयुक्त परिवार सम्पत्ति तथा उसकी आय में किसी भी सहदायिकी को अंश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। गिरिजा नन्दिनी बनाम बृजेन्द्र, ए० आई० आर० 1970 एस० सी० 1124 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक मिताक्षरा संयुक्त परिवार का सदस्य जिसे सहदायिक कहते हैं, अविभाजित रहता है, वह पारिवारिक सम्पत्ति में अपने अंश की कल्पना निश्चिततापूर्वक नहीं कर सकता। उसका संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अंश घटता-बढ़ता रहता है।
(3) विभाजन को प्रवर्तित कराने का अधिकार (Right to enforce partition) – संयुक्त परिवार के सभी सहदायिकों को अपने अंश के विभाजन की माँग करने का अधिकार है। यहाँ तक कि एक अवयस्क सहदायिकी भी संयुक्त परिवार सम्पत्ति विभाजन (Partition) की माँग कर सकता है। विभाजन की माँग का यह अधिकार उसकी इच्छा पर है, भले ही अन्य सहदायिक उससे सहमत हों या नहीं। विभाजन की माँग पिता, भाई तथा पितामह (दादा) से की जा सकती है। विभाजन की अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। इस अभिव्यक्ति का तरीका विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है। एक बार विभाजन की अभिव्यक्ति हो जाने पर परिवार की संयुक्त स्थिति परिवर्तित हो जाती है तथा पृथक् हो रहा सहदायिकी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि पश्चात्वर्ती करार द्वारा विभाजन का एकीकरण (Reunion) सम्भव है। [ पुट्टा रंगम्मा बनाम एम० एस० रंगम्मा, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1018.]
(4) अनधिकृत कार्य को रोकने का अधिकार (Right to restrain an unauthorised act)- एक सहदायिक, दीवार खड़ी करने या भवन निर्माण जैसे अन्य सहदायिक के अनधिकृत कार्य को रोकने का अधिकार रखता है। इस प्रकार यदि कोई सहदायिक संयुक्त सम्पत्ति पर दीवार खड़ी करता है या भवन निर्माण करता है जिससे किसी सहदायिक का संयुक्त उपभोग का अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसे कार्य से व्यथित पक्षकार उस अवैध निर्माण पर रोक लगा सकता है।
(5) लेखा माँगने का अधिकार (Right to demand accounts)- पारिवारिक निधि की वास्तविक स्थिति जानने के प्रयोजन से एक सहदायिकी, संयुक्त परिवार के प्रबन्धक से सम्बन्धित लेखा माँग सकता है।
गनपत बनाम अन्ना जी, 23 बम्बई 144 नामक वाद में संयुक्त परिवार की दुकान में एक सहदायिक को प्रवेश करने, लेखा पुस्तक का निरीक्षण करने तथा दुकान के प्रबन्धन में हिस्सा लेने से रोका गया। यह निर्णय दिया गया कि किसी सहदायिक को लेखा के निरीक्षण, दुकान में प्रवेश तथा दुकान के प्रबन्धन का पूरा अधिकार है।
(6) सहदायिक का संयुक्त परिवार सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार (Right of a Coparcener of alienation of joint family property) एक सहदायिक (Coparcener) को संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अपने अविभाज्य अंश के हस्तान्तरण का अधिकार अन्य सहदायिकों की सहमति से है। एक सहदायिकी, अन्य सहदायिकियों की सहमति से संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अपने अविभाज्य अंश का हस्तान्तरण कर सकता है। मद्रास, बम्बई तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के अनुसार एक सहदायिक संयुक्त परिवार में अपने अविभाज्य अंश का अन्तरण सहदायिकों की सहमति के बिना भी कर सकता है। शम्भू बनाम रामदेव, ए० आई० आर० 1982 इलाहाबाद 508 नामक बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि विधिक आवश्यकता तथा पूर्ववर्ती ऋणो के भुगतान के अभाव में उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का हस्तान्तरण शून्य है।
(7) हस्तान्तरण को निरस्त कराने का अधिकार (Right to set aside alienation)—पिता या कर्त्ता या अधिकार से परे किसी सहदायिकी द्वारा किये गये संयुक्त परिवार के (विक्रय, बन्धक) अन्तरण को निरस्त कराने का अधिकार किसी भी सहदायिक को है। परन्तु ऐसा हस्तान्तरण निरस्त कराने का अधिकार उस सहदायिक को नहीं है जिसका जन्म हस्तान्तरण (Alienation) के पश्चात् हुआ है।
अनधिकृत हस्तान्तरण से तात्पर्य निम्न हस्तान्तरण से है –
(1) विधिक आवश्यकता के अभाव में किया गया हस्तान्तरण;
(2) ऐसा संव्यवहार जो अवैध व्यय (खर्च) के लिए हुआ हो;
(3) ऐसा हस्तान्तरण (संव्यवहार) जो सम्पत्ति के लाभ के लिए न हो;
रामचन्द्रा बनाम बल्ला सिंह, ए० आई० आर० 1986 इलाहाबाद 193 नामक वाद में सहदायिकों में से एक ने विधिक आवश्यकता के अभाव में संयुक्त परिवार अचल सम्पत्ति के एक भाग को बेच दिया, यह निर्णय दिया गया कि अन्य सहदायिक इस विक्रय को निरस्त कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं।
(8) भरण-पोषण का अधिकार (Right of Maintenance)- सहदायिक की पत्नी तथा बच्चों को सहदायिकी निधि से भरण-पोषण का अधिकार है। सहदायिकी के सदस्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह संयुक्त परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का, उनको पत्नियों का, उनकी अविवाहिता पुत्रियों का भरण-पोषण संयुक्त परिवार की निधि से करे। भरण-पोषण में उनकी विधिक आवश्यकताओं को पूरा किये जाने का दायित्व है।
(9) सहदायिकी सम्पत्ति में अपना हित त्यागने का अधिकार (Right to renounce interest in coparcenary property) – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार एक सहदायिक, अन्य सहदायिकों के पक्ष में अपने हित को त्यागने का अधिकार रखता है। परन्तु इलाहाबाद तथा बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार अधिकारों का यह त्याग किसी विशिष्ट सहदायिक के पक्ष में न होकर सभी सहदायिकों के पक्ष में होना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार यदि किसी सहदायिक ने अपने हित का त्याग किया है तो वह हित (अंश) सभी सहदायिकों में न्यागत (Devolve) होगा जहाँ हित या अंश के त्याग के पश्चात् ऐसा सहदायिकी पुत्र उत्पन्न होता है जिसने संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अपने हित का त्याग किया है तो ऐसा पुत्र विभाजन का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा। [ सरथामबल बनाम सीरलान तथा अन्य (ए० आई० आर० 1981 मद्रास 59 ) ]
(10) उत्तरजीविता का अधिकार (Right of Survivorship)- एक सहदायिक का संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अविभाज्य अंश उसकी मृत्यु के पश्चात् अन्य जीवित महदायिकों में संयुक्त रूप से न्यागत (Devolve) हो जाता है अर्थात् उसके अंश को सभी जीवित सहदायिक संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे। यह उत्तराधिकार के अन्तर्गत न होकर उत्तरजीविता के अन्तर्गत होता है। हिन्दू विधि अवयस्क तथा वयस्क सहदायिक में कोई अन्तर नहीं रखती। मेन के अनुसार अविभाज्य संयुक्त हिन्दू परिवार में उत्तराधिकार का प्रश्न हो नहीं है।
प्रश्न 18. संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की विवेचना कीजिए तथा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति व पृथक् सम्पत्ति में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए।
अथवा
सहदायिकी सम्पत्ति के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
Explain Joint Hindu family properties and distinguish it from self acquired properties with examples.
Or
Give a brief account of the classification of coparcenary property.
उत्तर– संयुक्त परिवार सम्पत्ति या सहदायिकी सम्पत्ति उस सम्पत्ति कहते हैं जिसमें सभी सहदायिकों के स्वामित्व की एकता तथा हकों की सामूहिकता होती है। ऐसी सम्पत्ति में निम्न सम्मिलित हैं –
(1) पैतृक सम्पत्ति;
(2) संयुक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित सम्पत्ति ।
(3) सदस्यों की पृथक् सम्पत्ति जो सम्मिलित कोष में डाल दी गई है।
(4) संयुक्त परिवार की निधि से किसी या सभी सहदायिकों द्वारा अर्जित सम्पत्ति ।
भगवन्त पी० सुखाले बनाम दिगम्बर सुखाले, ए० आई० आर० (1986) एस० सी० 76 तथा शेर सिंह बनाम गम्दूर सिंह, ए० आई० आर० (1997) एस० सी० 1333 के वादों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति तब तक संयुक्त बनी रहती है, जब तक वह अस्तित्व में रहती है और विभाजित नहीं की जाती। संयुक्त परिवार की प्रास्थिति में विघटन हो जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता।
(1) पैतृक सम्पत्ति- पैतृक सम्पत्ति का तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जो पुरुष वंशानुक्रम से पुरुष क्रम में आती है। इस सम्पत्ति में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र जन्म से ही हक प्राप्त करते हैं। (याज्ञवल्क्य) उस सम्पत्ति को हिन्दू पुरुष अपने पिता, पितामह अथवा प्रपितामह से प्राप्त करता है अर्थात् अपने तीन उपर्युक्त पैतृक पूर्वजों से दान में प्राप्त सम्पत्ति ही पैतृक सम्पत्ति कहलाती है तथा केवल वे व्यक्ति जो उसमें जन्म से हक प्राप्त करते हैं, पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र हैं।
कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम पी० चेट्टीयार (1969) 71 आई० टी० आर० 601 (मद्रास) के वाद में यह निरूपित किया गया कि जहाँ दानपत्र में पिता द्वारा यह नहीं गत किया गया कि आदाता सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करेगा, वह सम्पत्ति आदाता की निर्बाध सम्पत्ति होगी जिसमें पुत्रों को जन्मत: कोई अधिकार नहीं उत्पन्न होगा।
(2) संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित सम्पत्ति– जहाँ संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा उनके संयुक्त परिश्रम तथा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति की सहायता से कोई सम्पत्ति अर्जित की जाती है, वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति अथवा सहदायिक सम्पत्ति हो जाती है।
हरीदास बनाम देव कुंवर बाई, 50 बाम्बे 443 के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सम्पत्ति संयुक्त परिवार के सदस्यों के संयुक्त श्रम से अर्जित की गई है, चाहे उसमें संयुक्त कोष की सहायता न ली गई हो तो भी वह किसी विपरीत उद्देश्य के अभाव में, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है।
श्रीमती स्वर्णलता बनाम कुलभूषण पाल, ए० आई० आर० (2014) दिल्ली 86 के मामले में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ संयुक्त हिन्दू परिवार के अन्तर्गत कर्ता के द्वारा कोई सम्पत्ति खरीदी जाती है अथवा कर्ता के द्वारा कोई सम्पत्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से खरीदी जाती है वहाँ ऐसी सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की ही सम्पत्ति मानी जायेगी, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
(3) ऐसी सम्पत्ति जो समान कोष में डाल दी गई है – यदि कोई स्वार्जित सम्पत्ति समान कोष में इस उद्देश्य से डाल दी गयी है कि अपने हक का परित्याग कर दे तो वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति हो जाती है, जो परिवार के सभी सदस्यों में विभाज्य है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उस उद्देश्य से कोई विचार अभिव्यक्त किया जाय। उसको समान कोप में डाल देना तथा उसमें एवं अन्य संयुक्त सम्पत्ति में कोई अन्तर न मानना इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि वह संयुक्त सम्पत्ति जैसी मान ली जाय। (लाल बहादुर बनाम कन्हैया लाल, 24 इला० 244 )
(4) संयुक्त परिवार की निधि से किसी या सभी सहदायिकों द्वारा अर्जित सम्पत्ति – संयुक्त परिवार की सम्पत्ति की सहायता से अर्जित की गई सम्पत्ति भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति कही जाती है। इस प्रकार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से प्राप्त आय का अर्जित किया जाना एवं अर्जित आय से नयी सम्पत्ति को खरीदना, किसी सम्पत्ति को बेचने अथवा बन्धक रखकर धनराशि का अर्जित करना अथवा उससे किसी नयी सम्पत्ति का खरौदना, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति कहलाती है।
परमानन्द बनाम सुदामा राम, ए० आई० आर० 1994 एच० पी० 87 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जहाँ कर्त्ता कोई सम्पत्ति अपने नाम से खरीदता है और यह नहीं कहता कि संयुक्त पारिवारिक राशि उस सम्पत्ति को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी वहाँ यह प्रमाण भार उसके ऊपर है कि वह साबित करे कि अपनी पृथक् आय से उसने वह सम्पत्ति खरोदो है। ऐसा प्रमाण न देने पर उसके द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति संयुक्त पारिवारिक राशि से खरोदी गई समझी जायेगी और वह संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति होगी।
पृथक् अथवा स्वार्जित सम्पत्ति का संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से भिन्नता – वह सम्पत्ति जो संयुक्त नहीं होती, पृथक् सम्पत्ति कहलाती है। पृथक् से आशय ऐसे परिवार से है। जो पहले संयुक्त था, किन्तु अब पृथक् हो चुका है। जब कोई व्यक्ति अपने भाइयों से अलग हो जाता है तो वह सम्पत्ति, जिसका वह उपयोग स्वयं करता है, भाइयों के प्रसंग में पृथक् सम्पत्ति कहलाती है। जहाँ तक उसके पुत्रों का सम्बन्ध है, उस सन्दर्भ में वह संयुक्त सम्पत्ति होगी।
(1) जो सम्पत्ति परिवार के अन्य सदस्यों के संयुक्त श्रम का परिणाम होती है, वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति कही जाती है जबकि अपने स्वयं के श्रम से अर्जित की गई सम्पत्ति पृथक् सम्पत्ति होगी।
जैसे– जहाँ संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बिना कोई सहायता लिये हुए स्वयं एक चिकित्सक के रूप में आयुर्वेदिक औषधि का व्यवसाय करता है, उससे बहुत सारी सम्पत्ति अर्जित करता है और उसकी आय से बन्धक पर ऋण भी देता है, और उससे भी आय एकत्र करता है वहाँ उसकी सम्पत्ति एवं आय को उसकी पृथक् सम्पत्ति माना जायेगा। [एस० ए० कुद्दूस बनाम एस० वीरप्पा, ए० आई० आर० (1994) कर्नाटक 20]
(2) वह सम्पत्ति जो अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह से दाय में प्राप्त होती है संयुक्त परिवार की सम्पत्ति कही जाती है जबकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से दाय में प्राप्त होती है तो पृथक् सम्पत्ति कही जाती है।
मदन लाल फूलचन्द्र जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० (1992) एस० सी० 1254 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई हिन्दू पुरुष पैतृक सम्पत्ति में एक अंश होने के साथ-साथ अपनी पृथक् सम्पत्ति भी रख सकता है। यदि वह कोई भूमि अपने चाचा से दाय में प्राप्त करता है और उसे उस सम्पत्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त है तो वह उसकी पृथक् सम्पत्ति होगी।
प्रश्न 19. संयुक्त परिवार के कर्त्ता की शक्तियों तथा उसकी स्थिति की चर्चा करें। क्या वह सम्पत्ति में संयुक्त परिवार के सहदायिकियों के अविभाज्य अंश का हस्तान्तरण कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में?
अथवा
संयुक्त हिन्दू परिवार में कर्त्ता की स्थिति की विवेचना कीजिए एवं उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
Explain powers and position of Karta in Joint Hindu Family. Whether he can mortgage the undivided share of other’s coparcenary property? If so when and under what circumstances.
Or
Discuss the position of the Karta of Hindu Joint Family and explain his rights and duties.
उत्तर– संयुक्त परिवार के अवयस्क सदस्यों तथा महिलाओं की देखभाल के लिए एक व्यवस्थापक की आवश्यकता सदैव रही है। संयुक्त परिवार के सन्दर्भ में ऐसे व्यवस्थापक को संयुक्त परिवार का कर्त्ता कहा जाता है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति तथा संयुक्त परिवार के कार्यकलापों के सन्दर्भ में संयुक्त परिवार के कर्त्ता को अत्यधिक विस्तृत अधिकार है। उसे संयुक्त परिवार का मुखिया कहा जाता है। उसकी स्थिति परिवार के मामलों में सर्वोच्च मानी जाती है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसे ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्य व्यवस्थापक को प्राप्त नहीं होते।
संयुक्त परिवार का कर्त्ता कौन हो सकता है? (Who can be Karta of Joint Family?) – पिता यदि जीवित है तो सामान्यतः वही अपने संयुक्त परिवार का कर्ता हो सकता है। न्यायालयों ने निर्णीत किया है कि सभी मामलों में पिता स्वाभाविक रूप से परिवार का कर्त्ता होता है। शिशुओं के मामले में संयुक्त पारिवारिक परिसम्पत्ति का आवश्यक रूप से कर्त्ता इस शिशु का पिता ही होता है। यदि संयुक्त परिवार में पिता जीवित नहीं है तथा संयुक्त परिवार में कई भाई हैं तो सबसे बड़ा भाई उस संयुक्त परिवार का कर्ता होगा। एक अवयस्क संयुक्त परिवार का कर्त्ता नहीं हो सकता। [ मोहिदीन इब्राहिम नाची बनाम मोहम्मद इब्राहिम साहिब (39 मद्रास 608) ]
सामान्यत: संयुक्त परिवार का वरिष्ठ सदस्य उस परिवार का कर्त्ता होता है परन्तु संयुक्त परिवार के अन्य सहदायिकों (Coparceners) की सहमति से कनिष्ठ सदस्य भी कर्त्ता हो सकता है। एक संयुक्त परिवार का कर्त्ता होने की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि वह संयुक्त परिवार का सहदायिक (Coparcener) हो अर्थात् यदि कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार का सहदायिक नहीं है तो वह उस संयुक्त परिवार का कर्ता नहीं हो सकता। इस प्रकार एक विधवा जो संयुक्त परिवार की सहदायिकी नहीं है, वह संयुक्त परिवार की कर्त्ता नहीं हो सकती। इस प्रकार एक माता कर्त्ता नहीं हो सकती तथा वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अवयस्क के अंश का अन्तरण नहीं कर सकती। परन्तु कर्त्ता की अनुपस्थिति में वह संरक्षक की क्षमता (हैसियत) से न्यायालय की अनुमति से सम्पत्ति में अवयस्क के अंश का अन्तरण (विक्रय आदि) कर सकती है। [वी० सीताराम राव बनाम विभीषनी प्रधान, ए० आई० आर० 1958 उड़ीसा 222 ]
संयुक्त हिन्दू परिवार में कर्त्ता की स्थिति (Position of Karta in Joint Hindu Family)– संयुक्त परिवार में कर्त्ता की स्थिति अद्वितीय है। संसार की किसी अन्य विधि व्यवस्था में कर्ता जैसा पद नहीं है। निर्धारित सीमाओं में कर्त्ता की शक्तियाँ असोमित हैं। संयुक्त परिवार में कर्त्ता की स्थिति की तुलना किसी न्यासी (Trustee), किसी अभिकर्त्ता तथा फर्म के भागीदार से नहीं की जा सकती।
इस सम्बन्ध में प्रिवी काउन्सिल का अवलोकन उल्लेखनीय हैं –
“ऐसे व्यक्ति (कर्त्ता) का सम्बन्ध स्वामी या अभिकर्ता या भागीदार जैसा या न्यासी जैसा नहीं है। वह उस अर्थ में किसी न्यास का न्यासी नहीं है कि वह परिवार की सम्पत्ति के संव्यवहारों के लिए किसी को उत्तरदायी एवं न ही उस पर यह दायित्व है कि वह वेतन भोगी अभिकर्त्ता या न्यासी की भाँति अपव्ययी बने।”
दायभाग विधि के अन्तर्गत संयुक्त परिवार के कर्त्ता तथा न्यास के न्यासी की स्थितियों में सन्निकटता है। कावेल ने टैगोर ला लेक्चर्स में यह अवलोकन किया कि कर्ता प्रतिनिधायी स्वामी (Representative Owner) है। इसका स्वतन्त्र अधिकार अन्य सहदायिकों के अधिकारों के सापेक्ष सीमित है तथा कर्त्ता का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण करने के उत्तरदायित्व तक विस्तृत है।
कर्ता संयुक्त परिवार को जो भी सेवाएँ प्रदान करता है वह वेतन रहित है यद्यपि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य उसके कठिन परिश्रम के लिए उसे वेतन देने पर सहमत हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो कर्त्ता को उस परिवार को दी जाने वाली सेवा के लिए दिया जाने वाला वेतन उसकी पृथक् सम्पत्ति होगी।
नरेन्द्र कुमार मोदी बनाम आयकर आयुक्त, ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 1953 नामक बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सामान्यत: संयुक्त परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य ही कर्त्ता होता है परन्तु संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति से परिवार के अगले वरिष्ठ सदस्य को कर्त्ता का दायित्व सौंपा जा सकता है।
कर्त्ता की शक्तियाँ शक्तियाँ प्राप्त हैं (Powers of Karta)- संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता को निम्न हैं-
(1) आय तथा व्यय से सम्बन्धित शक्ति या अधिकार;
(2) संयुक्त परिवार के व्यवसाय की व्यवस्था करने की शक्ति;
(3) पारिवारिक उद्देश्य के लिए कर्ज संविदा करने की शक्ति;
(4) संविदा या करार (अनुबन्ध) करने की शक्ति;
(5) पारिवारिक विवाद को माध्यस्थम् को सन्दर्भ करने की शक्ति;
(6) समझौता करने की शक्ति;
(7) उन्मुक्ति देने की शक्ति,
(8) कर्जों की अभिस्वीकृति करने की शक्ति;
(9) वाद या मुकदमों में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति तथा
(10) संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने की शक्ति।
(1) आय तथा व्यय से सम्बन्धित शक्ति (Power over Income and Expenditure) — यदि कर्त्ता संयुक्त परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए सम्पत्ति की आय को खर्च करता है तो उसे मितव्ययी होना आवश्यक नहीं है जैसा कि एक न्यास के न्यासी के लिए आवश्यक है। कर्त्ता संयुक्त परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण, शिक्षा, विवाह, श्राद्ध. तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए परिवार की सम्पत्ति को खर्च कर सकता है।
(2) संयुक्त परिवार के व्यवसाय की व्यवस्था या प्रबन्ध करने की शक्ति (Power to manage Joint Family Business) – संयुक्त परिवार के कर्त्ता को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संयुक्त परिवार के व्यवसाय का प्रबन्ध करे। वह संयुक्त परिवार के व्यवसाय की प्रगति के लिए सभी न्यायपूर्ण तथा आवश्यक कदम उठा सकता है।
(3) पारिवारिक उद्देश्य के लिए कर्ज संविदा करके कर्ज लेने की शक्ति (Power to contract debt for purpose of Joint Family)– संयुक्त परिवार का कर्त्ता संयुक्त परिवार के व्यवसाय के उद्देश्य से कर्ज लेने हेतु संविदा करने की शक्ति रखता है। तथा इस कर्ज से संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य उस सीमा तक उत्तरदायी होंगे जिस सीमा तक संयुक्त परिवार में उनका हित है। इस कर्ज से संयुक्त परिवार के वयस्क सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी बाध्य होंगे यदि वे कर्ज की संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से पक्षकार रहे हों या पश्चात्वर्ती समय में संविदा का अनुसमर्थन करते हैं। अवयस्क भी इस कर्ज से बाध्य होंगे यदि वे वयस्कता प्राप्त करने पर कर्ज की संविदा का अनुसमर्थन कर दें।
(4) संविदा करने की शक्ति (Power to Contract) संयुक्त परिवार का कर्त्ता संविदा करने की, रसीद देने की, समझौता करने की, संविदा से मुक्ति देने की संविदा कर सकता है परन्तु ऐसी संविदा परिवार के व्यापार या कारोबार के लिए आनुषंगिक ( सम्बन्धित : Incidental) हो।
(5) माध्यस्थम् को विवाद संदर्भित करने की शक्ति (Power to refer to Arbitration)- संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हितों के मामलों को कर्त्ता माध्यस्थम् (Arbitration) को सन्दर्भित कर सकता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य (जिसमें अवयस्क भी सम्मिलित हैं) इस माध्यस्थम के सन्दर्भ तथा पंचाट से बाध्य होंगे।
(6) समझौता करने की शक्ति (Power to enter into compromise)- संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के मामलों पर समझौता करने की शक्ति कर्त्ता को है। कर्त्ता को यह अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को वह संयुक्त परिवार को देय कर्ज से मुक्ति प्रदान करे। कर्त्ता बदले में या प्रतिफल के रूप में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को मूल्यवान वस्तु को किसी को नहीं दे सकता। परन्तु कर्त्ता को कर्जदारों के लेखा के सम्बन्ध में ब्याज या मूलधन के रूप में परिवार के हितों को समझौता कर व्यवस्थित करने का अधिकार है।
(7) उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति (Power to give discharge)– कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को देय वैध कर्ज से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है। यदि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अवयस्क है तो वह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अन्तर्गत छूट का लाभ नहीं ले सकता ( रति राय बनाम नैदर, 51 इलाहाबाद 435 ) ।
(8) ऋण की अभिस्वीकृति करने की शक्ति (Power to acknowledge the debt) संयुक्त परिवार के कर्ज की अभिस्वीकृति करने की शक्ति कर्त्ता को प्राप्त है। कर्त्ता संयुक्त परिवार के ऋण का आंशिक भुगतान भी कर सकता है जिससे परिसीमन अवधि विस्तारित होती है। कर्त्ता काल बाधित (Time barred) ॠण को पुनर्जीवित करने के प्रयोजन से नवीन वचन पत्र या बन्धक पत्र निष्पादित नहीं कर सकता।
(9) वाद में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति (Power to represent the suit ) संयुक्त परिवार की ओर से या संयुक्त परिवार के विरुद्ध लाये गये वाद में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति संयुक्त परिवार के कर्ता को प्राप्त है। इसलिए किसी वाद में संयुक्त परिवार के प्रत्येक या सभी सदस्यों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसे बाद में, जिसका प्रतिनिधित्व कर्त्ता करता है, न्यायालय द्वारा कोई आज्ञप्ति पारित की जाती है तो ऐसी आज्ञप्ति संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को उनके संयुक्त परिवार में हित की सीमा तक बाध्य करेगी जिसमें अवयस्क भी सम्मिलित है क्योंकि जहाँ तक अवयस्कों का प्रश्न है, कर्त्ता बाद में उनके हितों के लिए कार्य करता है तथा जहाँ तक वयस्क सदस्यों का प्रश्न है वहाँ वाद का प्रतिनिधित्व उनकी सहमति से करता है।
फती उन्निसा बेगम बनाम तमीरासा राज गोपाल चारीयूलू, ए० आई० आर० 1977 आन्ध्र प्रदेश 24 नामक बाद में यह प्रश्न उठा कि यदि एक विधवा, संयुक्त परिवार में अपने पति के हित को उत्तराधिकार में हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत प्राप्त करती है तो इससे संयुक्त परिवार में महिला की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे उत्तराधिकार के पश्चात् विधवा संयुक्त हिन्दू परिवार में अपने पति का स्थान पा लेती है तथा कर्त्ता संयुक्त परिवार में उसके हित का प्रतिनिधित्व पूर्व की भाँति करता रहता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के कारण महिला का संयुक्त परिवार में सौमित हित का पूर्ण हित में परिवर्तन से इस स्थिति (कत्ता के संयुक्त परिवार के बाद में प्रतिनिधित्व करने की शक्ति) में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता।
(10) कर्त्ता की सम्पत्ति के हस्तान्तरण की शक्ति (Power of Karta to alienate the property)-कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को निम्न शर्तों पर हस्तान्तरित (विक्रय आदि) कर सकता है –
(1) यदि सदस्य वयस्क है तो सभी वर्तमान सदस्यों की सहमति से
(2) वैध आवश्यकताओं के लिए (शिक्षा, स्वास्थ्य); तथा
(3) यदि संयुक्त परिवार का हस्तान्तरण संयुक्त परिवार के लाभ के लिए है।
यदि हस्तान्तरण संयुक्त परिवार के लाभ के लिए है तो अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं है।
संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में कुछ सीमाओं में कर्त्ता को सम्पत्ति के हस्तान्तरण की असीमित शक्ति है।
संयुक्त परिवार के लाभ के लिए कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है। (श्री शिव कुमारी बनाम इण्डियन ओवरसीज बैंक, ए० आई० आर० 1978 आन्ध्र प्रदेश 37) ।
संयुक्त परिवार के कर्त्ता को यह अधिकार है कि वह अपरिचितों को भेंट भी दे सकता है परन्तु यह उपहार या भेंट पवित्र प्रयोजनों के लिए होनी चाहिए।
विधिक आवश्यकता एक विस्तृत शब्दावली है। विधिक आवश्यकता साबित करने का दायित्व (भार) उस व्यक्ति पर है जिसको सम्पत्ति हस्तान्तरित की गई है। यदि विधिक आवश्यकता साबित नहीं हो पाती तो कर्त्ता (पिता) का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। [ज्वाला सिंह बनाम लक्ष्मण दास, ए० आई० आर० 1975 पंजाब तथा हरियाणा 188]
यदि पिता पैतृक सम्पत्ति को अपनी पुत्री को दान में दे देता है तो यह दान शून्यकरणीय न होकर शून्य होगा। [कन्डामल बनाम कन्डिया थापर, ए० आई० आर० 1977 एन० ओ० सी० (मद्रास) 220 ] यदि एक सहदायिकी संयुक्त परिवार में सम्पत्ति के अपने अंश को अपनी पत्नी के पक्ष में समर्पित (Surrender) कर देता है तो यह समर्पण (Surrender) अवैध होगा। (ए० आई० आर० 1989 कर्नाटक 31 ) ।
कृषि उपकरणों की खरीद या पौत्री की शादी के लिए किया गया खर्च विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत माना गया [धरम सिंह तथा अन्य बनाम साधु सिंह, ए० आई० आर० 1997 पंजाब तथा हरियाणा 198]
कर्त्ता के कर्तव्य तथा दायित्व (Duties and Liabilities of Karta) संयुक्त परिवार के कर्ता (प्रबन्धक) के प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्व निम्नलिखित हैं –
(1) लेखा प्रस्तुत करने का कर्तव्य;
(2) परिवार को प्राप्त होने वाले कजों को प्राप्त करने का कर्तव्य;
(3) उचित ढंग से खर्च करने का कर्तव्य;
(4) अन्य सहदाविकियों (Coparceners) की सहमति के बिना नवीन व्यापार प्रारम्भ न करने का कर्त्तव्य ; तथा
(5) सम्पत्ति के लाभ तथा विधिक आवश्यकता के अभाव में सहदायिको सम्पत्ति का हस्तान्तरण न करने का कर्तव्य
(1) लेखा प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य (Duty to render the accounts)– एक कत का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को संयुक्त परिवार को परिसम्पत्ति की आय तथा उस पर व्यय का विवरण प्रस्तुत करें जब तक कर्ता पर संयुक्त परिवार को सम्पत्ति के दुरुपयोग का आरोप न लगा हो, कर्त्ता संयुक्त परिवार से सम्बन्धित पूर्व संव्यवहारों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है। वह विभाजन के समय जो सम्पत्ति अस्तित्व में है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।
(2) संयुक्त परिवार को देय कर्ज को वसूलने का कर्त्तव्य (Duty to realise the debt due to the family)– कर्त्ता का यह कर्तव्य है कि वह संयुक्त परिवार को देय कर्ज वसूलने का प्रयास करे। यद्यपि उसे लेखों के समायोजन का अधिकार हैं परन्तु वह संयुक्त परिवार को देय कर्ज से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता।
(3) उचित (युक्तियुक्त रूप से खर्च करने का कर्त्तव्य (Duty to spend reasonably)– संयुक्त परिवार के कर्त्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह परिवार की निधि को सिर्फ परिवार के प्रयोजनों के लिए ही खर्च करे। अनावश्यक रूप से मितव्ययिता बरतने के लिए कर्त्ता बाध्य नहीं है। उसे उचित रूप से खर्च करना चाहिए। यदि वह उचित रूप से खर्च नहीं करता तथा उसका खर्च परिवार के अन्य सदस्यों से समर्थित नहीं है तो एकमात्र उपचार विभाजन की माँग करना है।
(4) संयुक्त परिवार के अन्य सहदायिकियों (Coparceners) की सहमति के बिना नवीन व्यवसाय प्रारम्भ न करने का कर्त्तव्य (Duty not to start new business without the consent of other coparceners) – नवीन व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से परामर्श या सहमति लेना कर्ता का प्रमुख कर्तव्य है क्योंकि संयुक्त परिवार के वयस्क तथा अवयस्क सदस्यों पर उनकी सहमति के अभाव में नवीन व्यवसाय का जोखिम कर्त्ता नहीं डाल सकता।
(5) परिसम्पत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के बिना संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को हस्तान्तरित न करने का कर्त्तव्य (Duty not to alienate coparcenary property except for legal necessity and benefit to the estate)- संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को विक्रय, बन्धक आदि के द्वारा हस्तान्तरित करने से पूर्व संयुक्त परिवार के वयस्क सदस्यों की सहमति लेना कर्त्ता का कर्त्तव्य है। परन्तु यदि कर्त्ता संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का हस्तान्तरण संयुक्त सम्पत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के अन्तर्गत करता है तो उसे अन्य सदस्यों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हस्तान्तरण सम्पत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के लिए है कि नहीं, उसकी कसौटी को सन्तुष्ट करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि हस्तान्तरण का संव्यवहार (Transaction) ऋजु (Fair) था तथा उन परिस्थितियों में जिनमें विक्रय किया गया था, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी विधिक आवश्यकता तथा सम्पत्ति के लाभ के लिए सम्पत्ति का हस्तान्तरण करता है।
कर्त्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं है (Karta has no power to make will)– संयुक्त परिवार के कर्त्ता को कुछ मामलों में संयुक्त परिवार के लघु अंश (Small Portion) को दान में देने का अधिकार है परन्तु वह संयुक्त परिवार के सदस्यों (Coparceners) की सहमति से भी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति वसीयत द्वारा अन्तरित नहीं कर सकता। [लक्ष्मी चन्द बनाम आनन्दी, 58 इण्डियन अपील 123]
कर्त्ता द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण शून्य अथवा शून्यकरणीय (Alienation of Joint Family Property void or voidable)– संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कर्ता द्वारा वसीयत या दान द्वारा किया गया हस्तान्तरण पूर्णतया शून्य (Void) है न कि शून्यकरणीय। परन्तु संयुक्त परिवार को सम्पत्ति का सम्पत्ति के लाभ या विधिक आवश्यकता के अभाव में किया गया अन्तरण संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के विकल्प पर शून्यकरणीय (Voidable) होता है।
पिता कर्त्ता के रूप में (Father as Karta)– मिताक्षरा विचारधारा के अनुसार कर्ता के रूप में पिता का संयुक्त परिवार के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अधिकार सामान्य कर्त्ता की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। पिता को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सामान्य कर्ता की अपेक्षा अतिरिक्त अधिकार या शक्ति प्राप्त है
(1) पिता को यह अधिकार है कि वह संयुक्त परिवार की अचल या चल सम्पत्ति को कर्ज चुकता करने के लिए बेच सकता है या बन्धक कर सकता है। यदि ऐसा कर्ज पूर्ववर्ती कर्ज (Antecedent debt) है तथा यह कर्ज अनैतिक या अवैध प्रयोजन से कलंकित नहीं है। सम्पत्ति के अन्तर्गत पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र के हित भी सम्मिलित हैं। [मधुसूदन बनाम भगवान, (1929) 33 बम्बई 444 ]
(2) प्रेम तथा स्नेह के लिए भेंट (दान) (Gift out of love and affection) – पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी पुत्री तथा दामाद के पक्ष में कठोर सीमा के अन्तर्गत दान कर सकता है। उसी प्रकार वह निकट स्नेही को भी दान दे सकता है। परन्तु एक अपरिचित या संयुक्त परिवार के सम्बन्धियों को किया गया दान शून्य (Void) है। पिता (कर्त्ता) ने सम्पूर्ण पैतृक अचल सम्पत्ति को अपनी पत्नी को दान में दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस दान को शून्य निर्णीत किया। [ कन्दमाल बनाम कन्दियाह थेयर, ए० आई० आर० 1977 एन० ओ० सी० 200 (मद्रास) ]
(3) पवित्र उद्देश्य के लिए दान (Gift for pious purposes) — एक पिता कर्त्ता को उपयुक्त सीमा के अन्तर्गत पवित्र उद्देश्यों के लिए पैत्रिक सम्पत्ति का दान करने की शक्ति प्राप्त है।