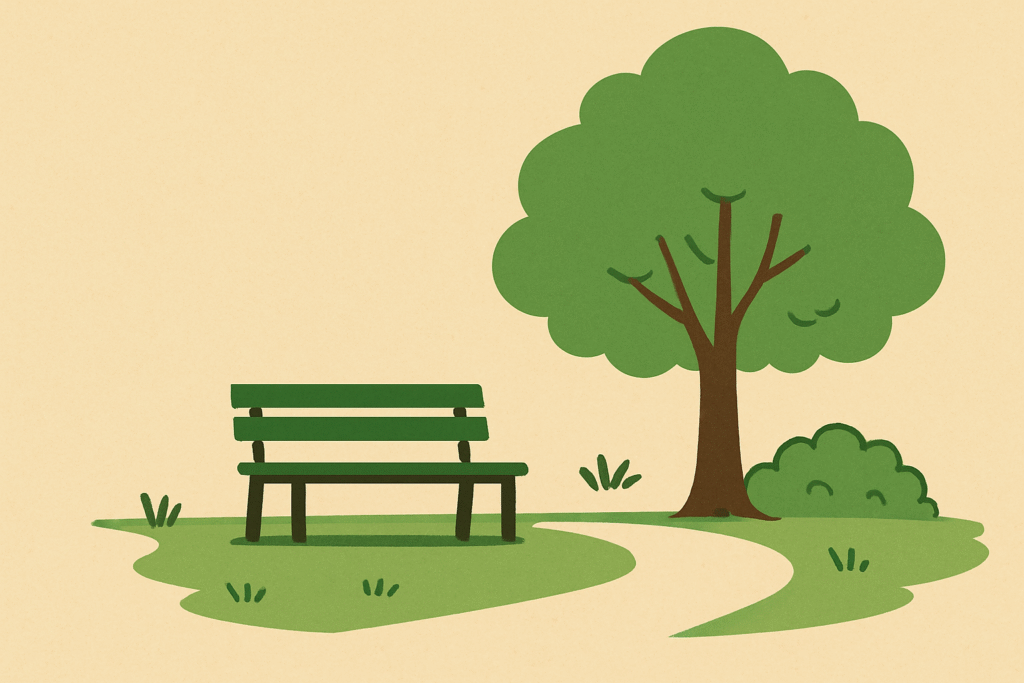प्रश्न: “उद्यान एवं सार्वजनिक पार्कों के संरक्षण और विकास से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विवेचना कीजिए।”
उत्तर:
भूमिका:
उद्यान एवं सार्वजनिक पार्क किसी भी नगर या नगर निगम क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में उद्यानों और सार्वजनिक पार्कों के संरक्षण एवं विकास हेतु अनेक कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य हरित क्षेत्रों की रक्षा, उनके सुव्यवस्थित विकास एवं नागरिकों को एक स्वच्छ, हरित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है।
1. संविधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या में भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण और स्वच्छ वातावरण को भी सम्मिलित किया है।
- अनुच्छेद 48-A – राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण और वनों की रक्षा और सुधार के लिए कार्य करे।
- अनुच्छेद 51-A(g) – प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे।
2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:
इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार है। यह अधिनियम पार्कों, उद्यानों एवं अन्य हरित क्षेत्रों की रक्षा में सहायक है।
3. नगर निगम अधिनियम / नगरपालिका अधिनियम:
राज्य सरकारों द्वारा लागू नगर निगम अधिनियमों में नगर निकायों को पार्कों की स्थापना, संरक्षण, रख-रखाव और विकास का उत्तरदायित्व दिया गया है। जैसे:
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959
- महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966
इन अधिनियमों के अंतर्गत अवैध कब्जा हटाने, सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता आदि के लिए नियम बनाए गए हैं।
4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (NGT Act):
NGT पर्यावरणीय मामलों में एक विशेष न्यायाधिकरण है। इसने कई निर्णयों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि पार्कों पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण न हो और सार्वजनिक हरित क्षेत्र सुरक्षित रहें।
प्रमुख निर्णय:
फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमिटी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) – इस मामले में NGT ने कहा कि पार्कों का उपयोग केवल मनोरंजन व हरियाली के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यावसायिक या निजी कार्यों के लिए।
5. न्यायिक दृष्टिकोण:
भारतीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर अपने निर्णयों में पार्कों की महत्ता को स्वीकार किया है। न्यायपालिका ने बार-बार यह दोहराया है कि सार्वजनिक पार्कों को नागरिकों की भलाई हेतु संरक्षित रखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण मामला:
MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001) – इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों को अवैध निर्माण से मुक्त रखने का निर्देश दिया।
6. राज्य स्तरीय अधिनियम और योजनाएँ:
कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पार्क विकास योजनाएं शुरू की हैं, जैसे:
- उत्तर प्रदेश पार्क विकास नीति
- दिल्ली ग्रीन पॉलिसी
- बृहनमुंबई महानगर पालिका की ओपन स्पेस नीति
इन योजनाओं के माध्यम से पार्कों के लिए धन का आवंटन, रख-रखाव के लिए समितियों का गठन, तथा जन-सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है।
7. जनभागीदारी और एनजीओ की भूमिका:
कानून के साथ-साथ कई स्वयंसेवी संगठन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पर्यावरण प्रेमी नागरिक पार्कों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार भी “पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप” (PPP) मॉडल के माध्यम से पार्कों का विकास कर रही है।
निष्कर्ष:
उद्यान एवं सार्वजनिक पार्क न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। उनके संरक्षण और विकास के लिए भारतीय विधि प्रणाली में पर्याप्त कानूनी प्रावधान हैं, किंतु इनका प्रभावी क्रियान्वयन, नागरिकों की जागरूकता और सरकारी इच्छाशक्ति आवश्यक है। न्यायपालिका की सक्रियता और जनसहभागिता के माध्यम से इन हरित धरोहरों को संरक्षित रखा जा सकता है।
प्रश्न 2: “नगर निगम अधिनियमों के अंतर्गत पार्कों और उद्यानों के रख-रखाव के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियों का विश्लेषण कीजिए।”
उत्तर:
भूमिका:
भारत के शहरी क्षेत्रों में उद्यान और सार्वजनिक पार्क नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, मनोरंजन, व्यायाम तथा मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इन हरित क्षेत्रों का विकास, रख-रखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करना नगर निकायों का एक प्रमुख दायित्व है। इस कार्य के लिए नगर निगम अधिनियमों में स्पष्ट प्रावधान हैं, जो संबंधित प्रशासनिक निकायों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हैं।
1. नगर निगम की कानूनी स्थिति:
नगर निगम संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत गठित होते हैं। यह संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को विधिक अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों की देखरेख के लिए सक्षम बनाता है। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग नगर निगम अधिनियम लागू हैं, जैसे:
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957
- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959
- बृहन्मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888
- कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976
इन अधिनियमों के अंतर्गत नगर निगमों को पार्कों एवं उद्यानों के संबंध में कई प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
2. पार्कों और उद्यानों के रख-रखाव हेतु प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ:
(क) योजना निर्माण और विकास:
नगर निगमों को यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के भौगोलिक, जनसंख्या और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार पार्कों की योजना बनाएं एवं उनका विकास करें।
(ख) भूमि का आरक्षण एवं उपयोग:
नगर निगमों को मास्टर प्लान के अंतर्गत हरित क्षेत्रों के लिए भूमि आरक्षित करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि वह भूमि अन्य किसी प्रयोजन में प्रयुक्त न हो।
(ग) रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण:
पार्कों की नियमित सफाई, पौधारोपण, बेंच, झूले, प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली आदि का रख-रखाव करना निगम की जिम्मेदारी है।
(घ) अवैध कब्जों को हटाना:
नगर निगमों को पार्कों पर अवैध अतिक्रमण, झुग्गी-झोपड़ी, दुकानें या निजी निर्माण को रोकना और हटाना होता है।
(ङ) बजट प्रावधान:
हर वित्तीय वर्ष में पार्कों और उद्यानों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित करना तथा उसके प्रभावी व्यय की निगरानी करना प्रशासन का कार्य है।
(च) नागरिक सहभागिता:
नगर निगम स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी संगठनों के सहयोग से पार्कों के विकास और रख-रखाव में जनभागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
(छ) सुरक्षा और निगरानी:
पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रहरियों की नियुक्ति करता है या कैमरा निगरानी की व्यवस्था करता है।
3. कानूनी प्रवर्तन शक्तियाँ:
नगर निगमों को अपने अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न दंडात्मक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे:
- अवैध अतिक्रमण पर जुर्माना लगाना
- पार्कों की भूमि पर अनधिकृत गतिविधियों को हटाना
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना
4. न्यायिक हस्तक्षेप और उत्तरदायित्व:
न्यायालयों ने नगर निगमों को यह याद दिलाया है कि पार्क केवल हरित सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से भी जुड़े हैं।
उदाहरण: MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगमों को पार्कों की रक्षा हेतु सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
निष्कर्ष:
नगर निगम अधिनियमों के तहत पार्कों और उद्यानों की देखरेख एक व्यापक प्रशासनिक दायित्व है। नगर निगमों को न केवल भौतिक संरचनाओं का निर्माण करना होता है, बल्कि उनके सतत संरक्षण, रख-रखाव और जनहित में उपयोग को भी सुनिश्चित करना होता है। प्रशासनिक कुशलता, बजट प्रबंधन, जनसहभागिता और न्यायिक मार्गदर्शन के माध्यम से यह कार्य प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। केवल तभी शहरी जीवन में हरियाली और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है।
प्रश्न:
“क्या नागरिकों को सार्वजनिक उद्यानों में प्रवेश और उपयोग का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? इस विषय में न्यायालयों के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए।”
उत्तर:
भूमिका:
सार्वजनिक उद्यान (Public Parks) केवल मनोरंजन और विश्राम के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे शहरी जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय संतुलन, और सामाजिक सहभागिता के लिए अनिवार्य तत्व हैं। प्रश्न यह है कि क्या नागरिकों को इन उद्यानों में प्रवेश और उपयोग का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संविधान और न्यायालयों की व्याख्या में निहित है।
1. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अधिकार:
भारतीय संविधान में नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से संबंधित कुछ व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत सार्वजनिक पार्कों तक पहुँच और उनके उपयोग का अधिकार भी व्याख्यायित किया गया है:
(क) अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि “स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार” अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है, और स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं हरित वातावरण इसका आवश्यक घटक है। सार्वजनिक उद्यानों का उपयोग इसी अधिकार के अंतर्गत आता है।
(ख) अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार:
यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्कों के उपयोग का समान अधिकार प्राप्त हो।
(ग) अनुच्छेद 15(2) – सार्वजनिक स्थलों पर पहुँच का अधिकार:
यह प्रावधान नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से मुक्त करता है, जिसमें सार्वजनिक पार्क भी सम्मिलित हैं।
2. न्यायालयों का दृष्टिकोण:
भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सार्वजनिक उद्यानों के उपयोग का अधिकार संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित है।
(i) MC Mehta v. Union of India (2001):
इस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों की रक्षा पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि पार्कों और हरित क्षेत्रों को नागरिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संरक्षित रखना आवश्यक है।
(ii) Municipal Corporation of Greater Mumbai v. Kamla Mills Ltd. (2001):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगमों का दायित्व है कि वे पार्कों को जनसामान्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति न दें।
(iii) K. Ramadas Shenoy v. Chief Officers, Town Municipal Council (1974):
इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय मास्टर प्लान के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि किसी भूमि को पार्क के रूप में आरक्षित किया गया है, तो उसे किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकता।
(iv) Intellectual Forum, Tirupathi v. State of A.P. (2006):
इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उद्यानों और प्राकृतिक स्थलों का उपयोग केवल विकास के नाम पर नहीं बदला जा सकता। यह प्राकृतिक संपत्तियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहनी चाहिए।
3. लोकहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से संरक्षण:
कई सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने लोकहित याचिकाओं के माध्यम से पार्कों की रक्षा के लिए न्यायालयों का रुख किया है। न्यायालयों ने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि की है।
4. सीमाएं और प्रतिबंध:
यद्यपि सार्वजनिक उद्यानों के उपयोग का अधिकार संवैधानिक है, फिर भी यह पूर्णतः निरंकुश नहीं है। प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, समय-सीमा और रख-रखाव के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे:
- निश्चित समय के लिए पार्क खुलना
- कुछ गतिविधियों पर रोक (जैसे शराब पीना, ध्वनि प्रदूषण)
- प्रवेश शुल्क (कुछ विशेष पार्कों में)
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अधिकारों को सीमित करना नहीं, बल्कि व्यवस्थापन करना होता है।
निष्कर्ष:
नागरिकों को सार्वजनिक उद्यानों में प्रवेश और उपयोग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15(2) के आलोक में प्राप्त है। न्यायपालिका ने भी इस अधिकार को मान्यता दी है और बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हरित क्षेत्रों तक पहुँच और उनके उपयोग को प्रतिबंधित करना नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह अधिकार न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए। अतः सार्वजनिक उद्यान केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से संरक्षित सामाजिक-सार्वजनिक संसाधन हैं।
प्रश्न:
“पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सार्वजनिक पार्कों की भूमिका और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कीजिए।”
उत्तर:
भूमिका:
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय संकट और विशेष रूप से 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् पारित किया गया एक व्यापक कानून है। इसका उद्देश्य वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीवों सहित सम्पूर्ण पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि पार्क शहरी पारिस्थितिकी में हरित क्षेत्र (green lungs) के रूप में कार्य करते हैं।
1. अधिनियम का उद्देश्य और प्रकृति:
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एक “छत्र कानून” (umbrella legislation) है, जो अन्य पर्यावरणीय कानूनों जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम आदि के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य है:
- पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारना,
- हानिकारक गतिविधियों को नियंत्रित करना,
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
सार्वजनिक पार्कों की भूमिका इन सभी उद्देश्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. सार्वजनिक पार्कों की पर्यावरणीय भूमिका:
- प्राकृतिक वायुप्रदूषण निवारक: पेड़ पौधे वायु में उपस्थित हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं।
- शहरी तापमान नियंत्रण: पार्क ‘heat islands’ को कम करते हैं।
- जैव विविधता संरक्षण: पार्क पक्षियों, कीटों और पौधों की अनेक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- जल संरक्षण: हरित क्षेत्र भूजल रिचार्ज में सहायक होते हैं।
इन्हीं कारणों से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पार्कों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
3. अधिनियम के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान:
(क) धारा 3 – केंद्र सरकार की शक्तियाँ:
सरकार को यह अधिकार है कि वह पर्यावरण की रक्षा हेतु नीतियाँ बनाए और दिशानिर्देश जारी करे। इसमें पार्कों की स्थापना, अवैध निर्माण की रोकथाम, और हरित क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित आदेश शामिल हो सकते हैं।
(ख) धारा 5 – प्रतिबंध और आदेश:
सरकार किसी भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगा सकती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो — जैसे पार्कों में वाणिज्यिक निर्माण, पेड़ों की कटाई या प्रदूषणकारी गतिविधियाँ।
(ग) धारा 7 और 8 – मानक और प्रतिबंध:
इन धाराओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो। यह पार्कों के प्रदूषण से बचाव के लिए उपयोगी है।
(घ) धारा 15 – दंडात्मक प्रावधान:
यदि कोई व्यक्ति या संस्था अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास या जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
4. न्यायिक दृष्टिकोण:
(i) MC Mehta v. Union of India
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हरित क्षेत्रों और सार्वजनिक पार्कों को संरक्षित करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का भाग है।
(ii) T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India
इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक हरित क्षेत्र, चाहे वह वन भूमि हो या नगरीय पार्क, पर्यावरण का हिस्सा है और उसकी रक्षा आवश्यक है।
5. प्रशासनिक अनुप्रयोग:
केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न गाइडलाइंस और निर्देश जारी करते हैं, जैसे:
- शहरों में हरित क्षेत्र न्यूनतम प्रतिशत में सुनिश्चित करना,
- पार्कों में प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध,
- वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व अनुमति।
6. नागरिक सहभागिता और जागरूकता:
इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है कि वे किसी पर्यावरणीय क्षति की शिकायत संबंधित बोर्ड/प्राधिकरण से कर सकते हैं। इसने सार्वजनिक पार्कों के संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
निष्कर्ष:
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 न केवल एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, बल्कि यह सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्वीकार करता है। यह अधिनियम सरकार, प्रशासन और नागरिकों – तीनों को उत्तरदायी बनाता है ताकि पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा हो सके। अतः यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक पार्कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित है।
प्रश्न:
“पार्कों में अवैध अतिक्रमण और उसके समाधान के लिए उपलब्ध विधिक उपायों की विवेचना कीजिए।”
उत्तर:
भूमिका:
पार्क और सार्वजनिक उद्यान किसी भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक सहभागिता और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। किंतु दुर्भाग्यवश, भारत के अनेक शहरों और कस्बों में पार्कों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण (Encroachment) एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु प्रभावी विधिक उपायों की समीक्षा आवश्यक है।
1. अवैध अतिक्रमण: स्वरूप और प्रभाव
(क) स्वरूप:
- झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण
- दुकानों व अस्थायी ढांचों का निर्माण
- धार्मिक या राजनीतिक स्थलों की स्थापना
- निजी पार्किंग या बाड़बंदी
(ख) प्रभाव:
- नागरिकों के उपयोग में बाधा
- हरित क्षेत्र की हानि
- पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन
- अपराध और अव्यवस्था की वृद्धि
2. विधिक दृष्टिकोण:
अवैध अतिक्रमण एक प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा है, जिस पर अनेक कानूनों और न्यायिक निर्णयों द्वारा रोक लगाई गई है।
3. समाधान हेतु प्रमुख विधिक उपाय:
(i) नगर निगम अधिनियम / नगर पालिका अधिनियम:
भारत के विभिन्न राज्यों में लागू नगर निगम अधिनियमों में निगमों को अधिकार प्राप्त हैं कि वे पार्कों पर अवैध कब्जे को हटाएं।
उदाहरण:
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 478 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्रदान की गई है।
(ii) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा की समाप्ति) अधिनियम, 1971:
इस अधिनियम के तहत सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों पर किए गए अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सक्षम अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।
(iii) भारतीय दंड संहिता (IPC):
- धारा 441 – आपराधिक अनधिकार प्रवेश (Criminal Trespass)
- धारा 447 – सार्वजनिक संपत्ति पर घुसपैठ की सजा
(iv) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:
यह अधिनियम सार्वजनिक हरित क्षेत्रों की रक्षा का अधिकार सरकार को देता है। पार्कों में अतिक्रमण को पर्यावरणीय अपराध माना जा सकता है।
(v) न्यायालय द्वारा निर्देशित उपाय:
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने अनेक मामलों में नगर निगमों को निर्देशित किया है कि वे पार्कों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करें और उसका सार्वजनिक उद्देश्य में उपयोग सुनिश्चित करें।
उदाहरण:
- MC Mehta v. Union of India – सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में पार्कों की भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
- Municipal Corporation of Greater Mumbai v. Kamla Mills Ltd. – कोर्ट ने कहा कि पार्कों की जमीन का वाणिज्यिक उपयोग संविधान और जनहित के विरुद्ध है।
4. व्यावहारिक समाधान:
(क) जनहित याचिका (PIL):
नागरिक या सामाजिक संगठन उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं।
(ख) स्थानीय निकायों की कार्रवाई:
नगर निगमों को समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने चाहिए और इसके लिए स्थायी निगरानी समितियाँ गठित करनी चाहिए।
(ग) नागरिक भागीदारी:
स्थानीय निवासियों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को सक्षम बनाकर निगरानी और शिकायत प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है।
(घ) मीडिया और सामाजिक जागरूकता:
सार्वजनिक पार्कों पर कब्जे को उजागर करना और जनमत तैयार करना भी एक प्रभावी उपाय है।
5. चुनौतियाँ:
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- अतिक्रमणकारियों की पुनर्वास समस्या
- प्रशासनिक उदासीनता
- जनसंख्या दबाव और भूमि की कमी
निष्कर्ष:
पार्कों में अवैध अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह नागरिकों के पर्यावरणीय अधिकारों का हनन भी है। भारत के विभिन्न विधिक प्रावधान — जैसे नगर निगम अधिनियम, सार्वजनिक परिसर अधिनियम, IPC, और पर्यावरण कानून — अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी इस दिशा में सख्त रहा है। आवश्यकता है कि इन प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।