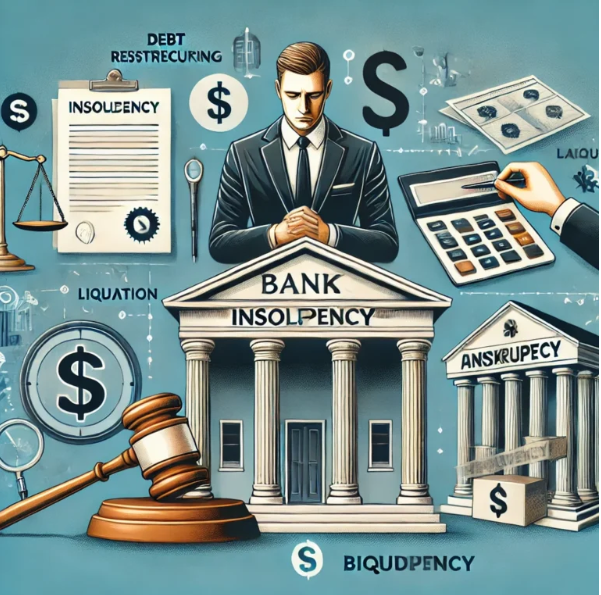भारतीय दिवालियापन कानून में क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी (Cross-Border Insolvency) के प्रावधानों का विश्लेषण
(Analysis of Cross-Border Insolvency Provisions under Indian Insolvency Law)
परिचय
क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी (Cross-Border Insolvency) का तात्पर्य उस स्थिति से है जब कोई देनदार (debtor) या उसकी संपत्ति एक से अधिक देशों में स्थित होती है, और उसे दिवालियापन से संबंधित मामलों का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकरण और विदेशी निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है।
भारत में यह मुद्दा विशेष रूप से तब उठता है जब:
- भारतीय कंपनियों की परिसंपत्तियाँ विदेशों में होती हैं, या
- विदेशी कंपनियाँ भारत में संचालन करती हैं और उनके विरुद्ध दिवालियापन की कार्यवाही होती है।
भारतीय कानून में वर्तमान स्थिति
1. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) में मौजूदा प्रावधान
IBC में क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी से संबंधित दो मुख्य धाराएँ हैं:
- धारा 234 (Section 234): भारत सरकार को किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय समझौता (bilateral agreement) करने का अधिकार देती है, ताकि क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी मामलों को सुचारु रूप से सुलझाया जा सके।
- धारा 235 (Section 235): समाधान पेशेवर (resolution professional) या लिक्विडेटर को यह अधिकार देती है कि वह विदेश की अदालत से सहायता मांगने हेतु NCLT की अनुमति प्राप्त कर सके।
वर्तमान समस्या:
- इन धाराओं के तहत कोई द्विपक्षीय समझौता अब तक लागू नहीं है।
- इन प्रावधानों को “अधूरे” (incomplete framework) के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे व्यावहारिक और पारदर्शी प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन नहीं करते।
भारत में प्रस्तावित समाधान – UNCITRAL Model Law
2. यूएनसिट्राल मॉडल कानून (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 1997)
भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) और IBBI ने यह सुझाव दिया है कि भारत को इस मॉडल कानून को अपनाना चाहिए। यह चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:
- पहचान (Access) – विदेशी प्रतिनिधियों को स्थानीय अदालत में पहुँच का अधिकार।
- पहचान (Recognition) – विदेशी दिवालियापन कार्यवाही को घरेलू न्यायालय द्वारा मान्यता देना।
- सहयोग (Cooperation) – घरेलू और विदेशी न्यायालयों एवं अधिकारियों के बीच सहयोग।
- समन्वय (Coordination) – एकाधिक न्यायक्षेत्रों में चल रही कार्यवाहियों के बीच तालमेल।
3. 2021 में प्रस्तावित ढाँचा
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी ढाँचा UNCITRAL मॉडल पर आधारित है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- “Foreign Main Proceeding” और “Foreign Non-Main Proceeding” की अवधारणाएँ
- NCLT को विदेशी कार्यवाहियों को मान्यता देने का अधिकार
- परिसंपत्तियों के संरक्षण हेतु स्वचालित स्थगन (automatic stay) का प्रावधान
- दोनों देशों की अदालतों के बीच सहयोग हेतु दिशानिर्देश
महत्त्व और आवश्यकता
- विदेशी निवेश की सुरक्षा: विदेशी लेनदारों और निवेशकों को विश्वास मिलता है कि भारतीय न्याय प्रणाली उनकी परिसंपत्तियों और अधिकारों की रक्षा करेगी।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए स्पष्टता: जब कंपनियाँ भारत और अन्य देशों में संचालन करती हैं, तो क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी नियम उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- संपत्तियों की अधिकतम वसूली: जब संपत्तियाँ एक से अधिक देशों में फैली होती हैं, तो ऐसा कानून वसूली को अधिक प्रभावी बनाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह वैश्विक कानून प्रणाली के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
भारत में चुनौतियाँ
- द्विपक्षीय संधियों की अनुपस्थिति
- विदेशी न्यायालयों से सहयोग की प्रक्रिया लंबी और जटिल
- संपत्ति की पहचान और नियंत्रण में कठिनाई
- मौजूदा NCLT प्रणाली का अधिभार
निष्कर्ष
भारत में क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी की व्यवस्था अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। यद्यपि IBC की धारा 234 और 235 इसका कानूनी आधार प्रदान करती हैं, परंतु इनकी प्रभावशीलता सीमित है। भारत को UNCITRAL Model Law को अपनाकर एक मजबूत, पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। यह न केवल विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और लेनदेन के लिए भारत को एक बेहतर गंतव्य बनाएगा।