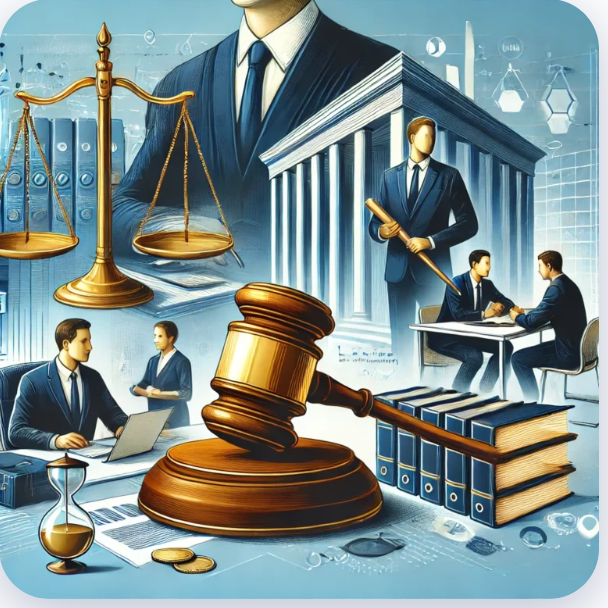दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India – IBBI) की संरचना, कार्य और शक्तियों पर प्रकाश
परिचय
भारत में वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने और दिवालियापन की प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC) लागू की गई। इस कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिवालियापन और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना की गई। IBBI इस कोड का प्रमुख नियामक निकाय है।
स्थापना और कानूनी आधार
- स्थापना: 1 अक्तूबर 2016
- कानूनी आधार: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 की धारा 188
- प्रकृति: एक स्वायत्त वैधानिक निकाय (Statutory Body)
IBBI की संरचना (Structure of IBBI)
IBBI का नेतृत्व एक अध्यक्ष (Chairperson) करता है और इसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसकी संरचना निम्न प्रकार है:
- एक अध्यक्ष – केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
- तीन सदस्य – केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, और विधि मंत्रालय से
- एक सदस्य – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से
- पाँच अन्य सदस्य – केंद्र सरकार द्वारा नामित, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक होते हैं
IBBI के प्रमुख कार्य (Functions of IBBI)
- दिवालियापन प्रक्रियाओं का विनियमन
- कॉर्पोरेट, साझेदारी और व्यक्तिगत इकाइयों की दिवालियापन प्रक्रिया को नियंत्रित और निरीक्षण करना।
- पंजीकरण और विनियमन
- निम्नलिखित इकाइयों को पंजीकृत करना और उनका नियमन करना:
a. Insolvency Professional Agencies (IPAs)
b. Insolvency Professionals (IPs)
c. Information Utilities (IUs)
- निम्नलिखित इकाइयों को पंजीकृत करना और उनका नियमन करना:
- नियमों और विनियमों का निर्माण
- IBC की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनियमन, प्रक्रिया और मानकों को निर्धारित करना।
- शिक्षा और प्रशिक्षण
- दिवालियापन पेशेवरों (IPs) को प्रशिक्षित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।
- सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना
- Information Utilities (IUs) के माध्यम से ऋण से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक और विश्वसनीय बनाना।
- शिकायत और अनुशासनात्मक कार्यवाही
- पंजीकृत संस्थाओं और पेशेवरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
- नीति निर्माण में भागीदारी
- केंद्र सरकार को दिवालियापन से संबंधित नीतियों पर परामर्श देना और सुधार हेतु सिफारिश करना।
IBBI की शक्तियाँ (Powers of IBBI)
- विनियम बनाने की शक्ति – IBC की विभिन्न धाराओं के तहत नियम व विनियम बनाना (जैसे – दिवालियापन प्रक्रिया, शुल्क, योग्यता मानदंड आदि)।
- निरीक्षण एवं जाँच की शक्ति – IPs, IPAs और IUs के कार्यकलापों का निरीक्षण करना और आवश्यकतानुसार जाँच करना।
- दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति – अनुशासनहीनता या नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित/रद्द करना, आर्थिक दंड लगाना।
- सूचना प्राप्त करने की शक्ति – किसी भी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक जानकारी माँगने का अधिकार।
- अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय – NCLT, RBI, SEBI जैसे अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।
महत्त्वपूर्ण योगदान
- IBC को लागू करके भारत की Ease of Doing Business रैंकिंग को सुधारने में भूमिका निभाई।
- समयबद्ध दिवालियापन प्रक्रिया को लागू किया (180 या 330 दिन की सीमा)।
- ऋणदाता-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया (Creditors in control)।
- ऋण की वसूली दर में सुधार हुआ।
निष्कर्ष
IBBI भारतीय दिवालियापन प्रणाली का स्तंभ है, जो न केवल नियमन करता है, बल्कि सुधारों, पारदर्शिता, और वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। इसकी संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ इसको एक प्रभावशाली और स्वतंत्र नियामक निकाय बनाती हैं, जो भारत की वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ और उत्तरदायी बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है।