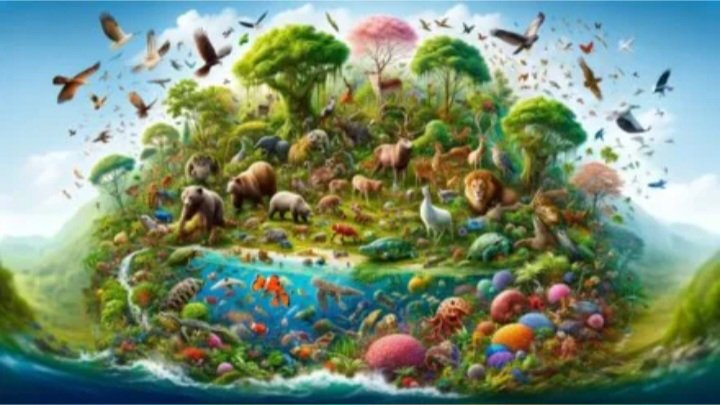जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
1. जैव विविधता (Biodiversity) क्या है?
उत्तर: जैव विविधता (Biological Diversity) का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, जिनमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। यह तीन स्तरों पर होती है:
- प्रजातिगत विविधता (Species Diversity) – विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु और पौधे।
- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity) – एक ही प्रजाति में मौजूद विभिन्न आनुवंशिक विशेषताएँ।
- पारिस्थितिकी विविधता (Ecosystem Diversity) – विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, जैसे वन, महासागर, नदी, घास के मैदान आदि।
2. जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है?
उत्तर: जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है क्योंकि:
- यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है।
- यह प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है।
- यह दवाओं, खाद्य पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है।
- यह आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
3. भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन-कौन से प्रमुख कानून लागू हैं?
उत्तर: भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई प्रमुख कानून लागू हैं, जैसे:
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)
- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927)
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan, 2008)
4. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) क्या है?
उत्तर: जैव विविधता अधिनियम, 2002 को भारत सरकार ने जैव संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक ज्ञान के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे के लिए लागू किया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता संधि (Convention on Biological Diversity – CBD) के अनुरूप बनाया गया था।
5. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) की स्थापना।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन।
- जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच और लाभों के बंटवारे (Access and Benefit Sharing – ABS) का प्रावधान।
- विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति आवश्यक।
6. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) क्या है और इसकी भूमिकाएँ क्या हैं?
उत्तर: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है, जो जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से संबंधित मामलों को नियंत्रित करती है। इसकी भूमिकाएँ हैं:
- जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
- विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों को जैव संसाधनों तक पहुँच की अनुमति देना।
- लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
7. जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committees – BMCs) क्या है?
उत्तर: जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) स्थानीय निकायों के तहत गठित की जाती हैं और इनका मुख्य कार्य जैव विविधता को संरक्षित करना और स्थानीय स्तर पर पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना होता है।
8. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उल्लंघन करने पर कोई दंड है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता अधिनियम, 2002 का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है:
- ₹10 लाख तक का आर्थिक दंड या
- 5 साल तक की कैद या दोनों।
9. भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन-कौन सी प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम हैं?
उत्तर: भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए कई प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे:
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan – 2008)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
10. क्या भारत में कोई जैव विविधता से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू हैं?
उत्तर: हाँ, भारत कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा है, जिनमें शामिल हैं:
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि (CBD) – 1992
- कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety) – 2000
- नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing) – 2010
- RAMSAR संधि (Wetland Conservation Treaty)
11. जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आम नागरिक क्या कर सकते हैं?
उत्तर: आम नागरिक निम्नलिखित तरीकों से जैव विविधता संरक्षण में योगदान दे सकते हैं:
- जंगलों की कटाई को रोकना और अधिक वृक्षारोपण करना।
- जैव विविधता से जुड़े कानूनों का पालन करना।
- पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना।
- जल और ऊर्जा का सतत उपयोग करना।
- अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (11-50)
11. जैव विविधता हानि (Biodiversity Loss) का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर: जैव विविधता हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- वनों की कटाई (Deforestation)
- पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution)
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
- अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी (Poaching & Wildlife Trafficking)
- पर्यावास विनाश (Habitat Destruction)
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species)
12. जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएँ हैं?
उत्तर: प्रमुख सरकारी योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया (National Mission for Green India)
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (National Wildlife Action Plan)
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan – NBAP)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत ईको-टूरिज्म योजना
13. जैव विविधता अधिनियम, 2002 में किस प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं?
उत्तर:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) को स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं।
- स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) को जैव विविधता पंजीकरण और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।
14. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) की सुरक्षा करता है?
उत्तर: हाँ, यह अधिनियम पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) की सुरक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि इसका अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग न हो।
15. भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots) हैं?
उत्तर: भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:
- हिमालयन हॉटस्पॉट
- इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट
- वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट
- सुंदरलैंड (सुंदरबन) हॉटस्पॉट
16. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत दंड और दायित्व क्या हैं?
उत्तर:
- किसी भी गैरकानूनी जैव संसाधन उपयोग के लिए ₹10 लाख तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल हो सकती है।
- यदि किसी कंपनी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
17. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं?
उत्तर:
- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) और वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) की स्थापना।
- लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau) का गठन।
18. क्या जैव विविधता संरक्षण में जैविक उद्यान (Biosphere Reserves) की भूमिका महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, जैविक उद्यान जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्राकृतिक पर्यावास को बनाए रखते हैं और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।
19. भारत में कितने जैविक उद्यान (Biosphere Reserves) हैं?
उत्तर: भारत में कुल 18 जैविक उद्यान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व
- सुंदरबन बायोस्फियर रिजर्व
- कच्छ बायोस्फियर रिजर्व
20. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Boards – SBBs) की क्या भूमिका है?
उत्तर:
- राज्य में जैव विविधता संरक्षण के लिए नियम लागू करना।
- अनुसंधान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- जैव विविधता हानि को रोकने के लिए नीतियाँ बनाना।
21. जैव विविधता संरक्षण में पारंपरिक समुदायों की क्या भूमिका है?
उत्तर: पारंपरिक समुदायों के पास पीढ़ियों से प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का खजाना होता है, जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण है।
22. क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, संगठन जैसे IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNEP (United Nations Environment Programme), WWF (World Wildlife Fund) जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
23. क्या भारत में जैव विविधता के लिए विशेष न्यायालय (Special Courts) हैं?
उत्तर: हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है।
24. भारतीय संविधान में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन-कौन से अनुच्छेद हैं?
उत्तर:
- अनुच्छेद 48A – राज्य को पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश।
- अनुच्छेद 51A(g) – नागरिकों का कर्तव्य कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।
25. क्या जैव विविधता का संरक्षण सतत विकास (Sustainable Development) से जुड़ा हुआ है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता संरक्षण सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है।
26. क्या कॉर्पोरेट क्षेत्र (Corporate Sector) जैव विविधता संरक्षण में योगदान कर सकता है?
उत्तर: हाँ, कई कंपनियाँ CSR (Corporate Social Responsibility) के तहत पर्यावरणीय स्थिरता कार्यक्रम चलाती हैं।
27. भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) हैं?
उत्तर: भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
28. जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक संधियाँ कौन-कौन सी हैं?
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि (CBD) – 1992
- RAMSAR संधि – 1971
- नागोया प्रोटोकॉल – 2010
29. क्या जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को प्रभावित करता है?
उत्तर: हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आवासों में बदलाव होता है, जिससे जैव विविधता को खतरा होता है।
30. भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन-कौन से वन्यजीव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
उत्तर:
- प्रोजेक्ट टाइगर
- प्रोजेक्ट एलीफेंट
- कछुआ संरक्षण कार्यक्रम
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (31-50)
31. जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन का क्या संबंध है?
उत्तर: जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, जिससे खाद्य शृंखला, जलवायु संतुलन, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।
32. क्या जैव विविधता संरक्षण में वनों की भूमिका है?
उत्तर: हाँ, वनों में कई प्रकार के पेड़-पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्मजीव रहते हैं, जो जैव विविधता का हिस्सा हैं। वनों के संरक्षण से न केवल जैव विविधता संरक्षित रहती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रित करता है।
33. क्या कृषि जैव विविधता (Agrobiodiversity) महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, कृषि जैव विविधता विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों, फलों और पालतू पशुओं के संरक्षण से संबंधित है। यह खाद्य सुरक्षा, पोषण और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बनाए रखने में सहायक है।
34. जैव विविधता और पारंपरिक औषधीय ज्ञान का क्या संबंध है?
उत्तर: पारंपरिक औषधीय ज्ञान, स्थानीय समुदायों द्वारा वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों के उपयोग पर आधारित होता है। जैव विविधता के संरक्षण से यह ज्ञान भी संरक्षित रहता है और आधुनिक दवाओं के विकास में मदद करता है।
35. क्या सतत पर्यटन (Sustainable Tourism) जैव विविधता को बचा सकता है?
उत्तर: हाँ, सतत पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करता है और स्थानीय समुदायों को जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।
36. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau – WCCB) क्या है?
उत्तर: WCCB भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है, जो वन्यजीव अपराधों को रोकने और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का कार्य करती है।
37. भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन-सा है?
उत्तर: भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालयन हॉटस्पॉट है, जो भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक फैला हुआ है।
38. बायोपायरेसी (Biopiracy) क्या है?
उत्तर: बायोपायरेसी तब होती है जब विदेशी कंपनियाँ या संस्थाएँ बिना अनुमति के किसी देश की जैव विविधता या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करती हैं।
39. क्या जैव विविधता संरक्षण आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता पर्यटन, जैव-औषधि, पारंपरिक चिकित्सा, और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
40. क्या जैव विविधता केवल स्थलीय (Terrestrial) जीवों तक सीमित है?
उत्तर: नहीं, जैव विविधता स्थलीय (Terrestrial) और जलीय (Aquatic) दोनों पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
41. क्या जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना जानते हैं।
42. क्या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services) जैव विविधता से जुड़ी होती हैं?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती है, जैसे कि परागण, जल शुद्धिकरण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, और जलवायु संतुलन।
43. क्या जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए खतरा है?
उत्तर: हाँ, जलवायु परिवर्तन से पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं और पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है।
44. जैव विविधता में सबसे अधिक योगदान देने वाले कारक कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
- जलवायु
- भौगोलिक विविधता
- पारिस्थितिक स्थितियाँ
- पारंपरिक कृषि और वन संरक्षण
45. क्या जैव विविधता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता पूरे विश्व के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे वैश्विक स्तर पर संरक्षित करने की आवश्यकता है।
46. क्या भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पेटेंट कानूनों का भी ध्यान रखा जाता है?
उत्तर: हाँ, यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी जैव संसाधन या पारंपरिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग बिना उचित अनुमति और लाभ साझा किए न किया जाए।
47. जैव विविधता हानि के प्रमुख कारण क्या हैं?
उत्तर:
- वनों की कटाई
- अवैध शिकार
- प्रदूषण
- जलवायु परिवर्तन
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ
48. जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन-कौन सी वैश्विक पहलें (Global Initiatives) की गई हैं?
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि (CBD)
- कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol)
- नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)
- RAMSAR संधि
49. क्या जल संसाधनों का संरक्षण जैव विविधता के लिए आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, जल संसाधनों का संरक्षण जलीय जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
50. क्या शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम जैव विविधता संरक्षण में मदद कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम लोगों को जैव विविधता संरक्षण के महत्व को समझाने और इसे बचाने के तरीकों के बारे में जागरूक करने में मदद करते हैं।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (51-100)
51. क्या भारत में जैव विविधता अधिनियम, 2002 स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता अधिनियम, 2002 स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है। यह जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग में उनके लिए लाभ साझा करने की व्यवस्था करता है।
52. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas – ESA) क्या होते हैं?
उत्तर: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है और जिन्हें मानवीय हस्तक्षेप से विशेष सुरक्षा दी जाती है, जैसे पश्चिमी घाट और सुंदरबन।
53. क्या जैव विविधता संरक्षण का संबंध सतत विकास (Sustainable Development) से है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता सतत विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखती है।
54. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA) क्या है?
उत्तर: NBA भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग की निगरानी करती है।
55. जैव विविधता में पशु और पौधों की क्या भूमिका होती है?
उत्तर: पशु और पौधे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं, जैसे परागण, खाद्य श्रृंखला बनाए रखना, कार्बन अवशोषण, और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना।
56. क्या जैव विविधता केवल प्राकृतिक वनों तक सीमित है?
उत्तर: नहीं, जैव विविधता कृषि भूमि, जल निकायों, शहरी क्षेत्रों, और यहां तक कि मरुस्थलों में भी पाई जाती है।
57. क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है?
उत्तर: हाँ, यह अधिनियम भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जो जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
58. क्या जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots) केवल भारत में ही हैं?
उत्तर: नहीं, जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं – हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट, और सुंडालैंड।
59. क्या समुद्री जैव विविधता भी महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, समुद्री जैव विविधता महासागरों, समुद्रों और तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
60. क्या जैव विविधता संरक्षण में सरकारों की भूमिका होती है?
उत्तर: हाँ, सरकारें कानून बनाकर, नीतियाँ लागू करके, और संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जैव विविधता को सुरक्षित रखती हैं।
61. क्या भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय योजना है?
उत्तर: हाँ, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (National Biodiversity Action Plan – NBAP) लागू है।
62. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकरण आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, यदि कोई कंपनी या व्यक्ति जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) में पंजीकरण कराना होगा।
63. भारत में कितने बायोस्फीयर रिज़र्व (Biosphere Reserves) हैं?
उत्तर: भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, जैसे नीलगिरि, सुंदरबन, और नोकरेक।
64. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 परंपरागत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है?
उत्तर: हाँ, यह अधिनियम पारंपरिक कृषि ज्ञान और जैव संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
65. क्या नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है?
उत्तर: हाँ, नागोया प्रोटोकॉल जैव संसाधनों के उचित उपयोग और लाभ साझा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
66. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत कोई दंड प्रावधान है?
उत्तर: हाँ, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास और आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
67. क्या वैश्विक तापमान वृद्धि (Global Warming) जैव विविधता को प्रभावित कर रही है?
उत्तर: हाँ, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि से कई प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।
68. क्या सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
उत्तर: हाँ, सरकार विभिन्न संरक्षण योजनाओं, अनुसंधान परियोजनाओं, और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देती है।
69. क्या पारिस्थितिकीय बहाली (Ecological Restoration) जैव विविधता संरक्षण का एक हिस्सा है?
उत्तर: हाँ, पारिस्थितिकीय बहाली उन पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करने का कार्य है जो मानवीय हस्तक्षेप या प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गए हैं।
70. क्या भारत में जैव विविधता रजिस्टर (Biodiversity Register) तैयार किया जाता है?
उत्तर: हाँ, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार किया जाता है।
71. क्या अपशिष्ट प्रबंधन जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा है?
उत्तर: हाँ, अपशिष्ट प्रबंधन जल, भूमि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके जैव विविधता की रक्षा करता है।
72. जैव विविधता हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
उत्तर:
- वन संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन नियंत्रण
- सतत कृषि
- जागरूकता अभियान
73. क्या जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए जीन बैंक (Gene Bank) बनाए जाते हैं?
उत्तर: हाँ, जीन बैंक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं।
74. क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैव विविधता को प्रभावित करता है?
उत्तर: हाँ, अवैध व्यापार और वनों की अंधाधुंध कटाई जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं।
75. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से संबंधित है?
उत्तर: हाँ, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परियोजनाओं के जैव विविधता पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (76-100)
76. क्या शहरीकरण जैव विविधता को प्रभावित करता है?
उत्तर: हाँ, शहरीकरण वनों की कटाई, भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण जैव विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
77. क्या पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services) जैव विविधता से जुड़ी होती हैं?
उत्तर: हाँ, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ, जैसे कि वायु और जल शुद्धिकरण, मिट्टी की उर्वरता, और परागण, जैव विविधता पर निर्भर करती हैं।
78. क्या भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कर (Tax) लगाया जाता है?
उत्तर: हाँ, कुछ राज्यों में जैव विविधता संरक्षण निधि (Biodiversity Conservation Fund) के लिए कर लगाया जाता है, जिससे जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
79. क्या राष्ट्रीय वन नीति (National Forest Policy) जैव विविधता संरक्षण में सहायक है?
उत्तर: हाँ, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
80. क्या भारत में जल जैव विविधता (Aquatic Biodiversity) के लिए कोई कानून है?
उत्तर: हाँ, जल अधिनियम, 1974 और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम जल जैव विविधता संरक्षण में मदद करते हैं।
81. क्या जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, क्योंकि स्थानीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक होते हैं, उनकी भागीदारी जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण होती है।
82. क्या भारत में बाघ परियोजना (Project Tiger) जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है?
उत्तर: हाँ, यह भारत में बाघों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है।
83. क्या वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau – WCCB) जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है?
उत्तर: हाँ, WCCB अवैध वन्यजीव व्यापार और जैव संसाधनों की तस्करी को रोकने में मदद करता है।
84. क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैव विविधता को प्रभावित करते हैं?
उत्तर: हाँ, पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएँ कभी-कभी प्राकृतिक आवासों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में इनका प्रभाव कम होता है।
85. क्या भारत में पर्यावरणीय न्यायाधिकरण (Environmental Tribunal) जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हैं?
उत्तर: हाँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है।
86. क्या ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972’ जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करता है?
उत्तर: हाँ, यह अधिनियम राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, और संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करता है।
87. क्या जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नष्ट कर सकता है?
उत्तर: हाँ, जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, तापमान बढ़ता है, और कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं।
88. क्या भारत में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून हैं?
उत्तर: हाँ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं।
89. क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत अनुसंधानकर्ताओं को अनुमति लेनी होती है?
उत्तर: हाँ, यदि कोई विदेशी अनुसंधानकर्ता जैव संसाधनों का अध्ययन करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमति लेनी होगी।
90. क्या औद्योगिक विकास जैव विविधता के लिए खतरा है?
उत्तर: हाँ, औद्योगिक विकास से प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है।
91. क्या भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त होती है?
उत्तर: हाँ, भारत को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF), और अन्य संगठनों से सहायता मिलती है।
92. क्या जलीय जीवों के संरक्षण के लिए कोई विशेष परियोजना है?
उत्तर: हाँ, डॉल्फिन संरक्षण परियोजना और मछली पालन संरक्षण योजना भारत में जलीय जैव विविधता की रक्षा के लिए चलाई जाती हैं।
93. क्या जैव विविधता संरक्षण में शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हाँ, लोगों को जैव विविधता के महत्व और संरक्षण उपायों के बारे में जागरूक करने से इसे बचाया जा सकता है।
94. क्या भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कोई पुरस्कार दिए जाते हैं?
उत्तर: हाँ, भारत सरकार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और बी.एन.एच.एस. पुरस्कार जैसे सम्मान प्रदान करती है।
95. क्या जैव विविधता संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है?
उत्तर: हाँ, निजी कंपनियाँ स्थायी व्यापार प्रथाओं, CSR गतिविधियों, और संरक्षण परियोजनाओं में योगदान देकर जैव विविधता संरक्षण में सहायता कर सकती हैं।
96. क्या जैव विविधता संरक्षण में सतत कृषि (Sustainable Agriculture) का योगदान है?
उत्तर: हाँ, जैविक खेती, मिश्रित फसल प्रणाली, और जल संरक्षण तकनीकें जैव विविधता संरक्षण में सहायक होती हैं।
97. क्या राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता संरक्षण में सहायक हैं?
उत्तर: हाँ, ये संरक्षित क्षेत्र वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षित रखते हैं।
98. क्या जनसंख्या वृद्धि जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है?
उत्तर: हाँ, अधिक जनसंख्या के कारण भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैव विविधता को नुकसान पहुँचाता है।
99. क्या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है?
उत्तर: हाँ, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
100. क्या किसी व्यक्ति को जैव विविधता संरक्षण में योगदान देने का अधिकार है?
उत्तर: हाँ, कोई भी व्यक्ति वृक्षारोपण, जैव संसाधनों का सतत उपयोग, स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर संरक्षण प्रयासों में योगदान दे सकता है।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (101-120)
101. जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखता है, जैविक संसाधनों को सुरक्षित रखता है, और पारिस्थितिकी सेवाओं (जैसे परागण, जल शुद्धिकरण, वायु गुणवत्ता सुधार) को सुनिश्चित करता है। जैव विविधता मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा, औषधीय अनुसंधान और जलवायु संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इसके संरक्षण से प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सकता है, और पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ बेहतर रूप से कार्य कर सकती हैं।
102. भारत में जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख कानून कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख कानून लागू हैं:
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 – जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 – संकटग्रस्त प्रजातियों और राष्ट्रीय उद्यानों की रक्षा करता है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 – वनों के अतिक्रमण और अनियंत्रित कटाई को रोकता है।
- पंचायती राज अधिनियम, 1996 (PESA Act) – आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण का अधिकार देता है।
103. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना – विदेशी कंपनियों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भारतीय जैव संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) – राज्य स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग की देखरेख करता है।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) – स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के दस्तावेजीकरण और संरक्षण का कार्य करता है।
- पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा – बायोपाइरेसी (Biopiracy) को रोकने और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए।
- विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध – जैव संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए NBA की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
104. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का कार्य क्या है?
उत्तर:
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- विदेशी कंपनियों और अनुसंधानकर्ताओं को जैव संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति देना।
- जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना।
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना।
- बायोपाइरेसी और अवैध जैव संसाधन व्यापार को रोकना।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के साथ समन्वय बनाकर जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना।
105. क्या जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है?
उत्तर:
हाँ, स्थानीय समुदाय जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में किया जा सकता है। भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का गठन किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर जैव संसाधनों के संरक्षण और प्रलेखन में मदद करता है।
106. भारत में कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण संधियों का पालन किया जाता है?
उत्तर:
भारत कई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण संधियों का पालन करता है, जिनमें प्रमुख हैं:
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD), 1992 – जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- रामसर सम्मेलन, 1971 – आर्द्रभूमि (Wetlands) और जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए।
- CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), 1973 – संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है।
- बॉन कन्वेंशन, 1979 – प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित संधि।
107. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का जैव विविधता संरक्षण में क्या योगदान है?
उत्तर:
यह अधिनियम भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना।
- शिकार और वन्यजीव व्यापार पर प्रतिबंध।
- पाँच अनुसूचियों (Schedules) के तहत जीवों की सुरक्षा।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) का गठन।
108. जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की भूमिका क्या है?
उत्तर:
राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यहाँ मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (गैंडा संरक्षण के लिए), सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (बंगाल टाइगर के लिए), और गिर राष्ट्रीय उद्यान (एशियाई शेरों के लिए) जैसे कई संरक्षित क्षेत्र हैं।
109. जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं:
- प्राकृतिक आवासों का विनाश – बर्फीले क्षेत्रों के पिघलने और वर्षा चक्र में बदलाव से कई प्रजातियाँ संकट में आ जाती हैं।
- प्रजातियों का विलुप्त होना – बढ़ते तापमान और बदलते पारिस्थितिकीय संतुलन के कारण कई जीव विलुप्त हो सकते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि – बाढ़, सूखा और समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं।
110. सतत विकास (Sustainable Development) जैव विविधता संरक्षण में कैसे मदद करता है?
उत्तर:
सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत जैव संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग किया जाता है, जिससे जैव विविधता संरक्षित रहती है। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (111-130)
111. पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) जैव विविधता संरक्षण में कैसे सहायक है?
उत्तर:
पारंपरिक ज्ञान स्थानीय समुदायों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित किया गया वह ज्ञान है जो जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण में सहायक होता है। उदाहरण के लिए:
- औषधीय पौधों का ज्ञान – विभिन्न वनस्पतियों का औषधीय उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है।
- खेती की पारंपरिक विधियाँ – स्थानीय किसानों द्वारा अपनाई गई जैविक कृषि विधियाँ भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं।
- जंगल और जल स्रोतों का संरक्षण – आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों से वनों और जल स्रोतों को बचाते हैं।
- बायोपाइरेसी से सुरक्षा – पारंपरिक ज्ञान को बायोपेटेंटिंग (Biopatenting) और बायोपाइरेसी से बचाने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।
112. जैव विविधता रजिस्टर (People’s Biodiversity Register – PBR) क्या है?
उत्तर:
जैव विविधता रजिस्टर (PBR) स्थानीय जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का एक दस्तावेजीकरण है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैव संसाधनों की जानकारी को संरक्षित करना और बायोपाइरेसी से बचाना है। इसे जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें वनस्पति, जीव-जंतु, औषधीय पौधे, कृषि प्रजातियाँ और पारंपरिक ज्ञान शामिल होते हैं।
113. क्या जैव विविधता केवल भूमि तक ही सीमित है, या इसमें समुद्री जैव विविधता भी शामिल है?
उत्तर:
नहीं, जैव विविधता केवल भूमि तक सीमित नहीं है। इसमें समुद्री जैव विविधता (Marine Biodiversity) भी शामिल होती है, जिसमें समुद्रों, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और जीव-जंतु शामिल हैं।
समुद्री जैव विविधता के उदाहरण:
- कोरल रीफ (Coral Reefs) – ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- मैंग्रोव जंगल (Mangrove Forests) – तटीय क्षेत्रों में जल स्तर को संतुलित रखते हैं।
- समुद्री जीव – मछलियाँ, कछुए, व्हेल, डॉल्फिन, केकड़े, झींगे आदि समुद्री जैव विविधता के प्रमुख घटक हैं।
समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) नीति और राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता कार्य योजना को लागू किया गया है।
114. जैव विविधता को खतरा पहुंचाने वाले प्रमुख कारण क्या हैं?
उत्तर:
जैव विविधता को निम्नलिखित कारणों से गंभीर खतरा है:
- वनों की कटाई (Deforestation) – प्राकृतिक आवासों के विनाश से कई जीव विलुप्त हो जाते हैं।
- शहरीकरण और औद्योगीकरण – प्राकृतिक संसाधनों का अति-दोहन और प्रदूषण जैव विविधता को नष्ट करता है।
- जलवायु परिवर्तन (Climate Change) – तापमान वृद्धि, वर्षा परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- बायोपाइरेसी (Biopiracy) – बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का अवैध रूप से दोहन करती हैं।
- अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार – कई दुर्लभ प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
115. बायोपाइरेसी (Biopiracy) क्या है? भारत में इसका कोई उदाहरण दीजिए।
उत्तर:
बायोपाइरेसी (Biopiracy) तब होती है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या शोध संस्थाएँ स्थानीय जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का अवैध रूप से उपयोग करके उस पर बायोपेटेंट प्राप्त कर लेती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को कोई लाभ नहीं मिलता।
भारत में बायोपाइरेसी के उदाहरण:
- नीम (Azadirachta indica) – एक विदेशी कंपनी ने नीम के कीटनाशक गुणों पर पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे चुनौती दी और पेटेंट रद्द कर दिया गया।
- हल्दी (Turmeric) – हल्दी के औषधीय गुणों पर भी अमेरिका में पेटेंट कराया गया था, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा कानूनी लड़ाई जीतने के बाद रद्द किया गया।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत भारत में बायोपाइरेसी को रोकने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) कार्यरत है।
116. क्या जैव विविधता को बचाने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन (Ecotourism) एक प्रभावी उपाय है?
उत्तर:
हाँ, पारिस्थितिकी पर्यटन (Ecotourism) एक प्रभावी उपाय है क्योंकि यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं:
- स्थानीय समुदायों को रोजगार मिलता है – जिससे वे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करते हैं।
- जागरूकता बढ़ती है – लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं।
- सरकार को वित्तीय सहायता मिलती है – संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव बेहतर होता है।
भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है।
117. जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots) क्या होते हैं? भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं?
उत्तर:
जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वे गंभीर रूप से खतरे में होते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट को पहचानने के लिए दो मानदंड होते हैं:
- क्षेत्र में कम से कम 1,500 स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए।
- क्षेत्र का कम से कम 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका हो।
भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:
- हिमालय (Himalayas)
- पश्चिमी घाट (Western Ghats)
- इंडो-बर्मा क्षेत्र (Indo-Burma Region)
- सुंदरबन और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (Sundaland including Nicobar Islands)
118. भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
उत्तर:
भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण हेतु कई योजनाएँ चलाई हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP)
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)
- मेक इन इंडिया के तहत जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB)
119. पारिस्थितिक संतुलन (Ecological Balance) और जैव विविधता का क्या संबंध है?
उत्तर:
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। प्रत्येक जीव पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका निभाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ सुचारू रूप से चलती हैं।
120. क्या बायोटेक्नोलॉजी जैव विविधता संरक्षण में सहायक हो सकती है?
उत्तर:
हाँ, बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnology) के माध्यम से विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण, जैविक खेती और पर्यावरण अनुकूल जैव उत्पादों का विकास संभव है। जीवाणु और फफूंद आधारित जैव कीटनाशकों का उपयोग रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर किया जा सकता है, जिससे जैव विविधता की रक्षा होती है।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (121-150)
121. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत “लोकतंत्र में जैव विविधता का संरक्षण” कैसे सुनिश्चित किया गया है?
उत्तर:
जैव विविधता अधिनियम, 2002 में लोकतांत्रिक तरीके से जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। यह विधेयक स्थानीय समुदायों, आदिवासियों, और अन्य क्षेत्रों को उनके पारंपरिक ज्ञान के इस्तेमाल का अधिकार देता है, जो जैव विविधता के संरक्षण में मदद करते हैं।
- पारिस्थितिकी-समिति (BMC) – समुदायों को जैव विविधता प्रबंधन के निर्णयों में शामिल किया गया है।
- संरक्षण और प्रबंधन योजना (Conservation and Management Plans) – इस योजना में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए समुदायों को जिम्मेदारी दी जाती है।
122. जैव विविधता को बचाने में पारंपरिक ज्ञान का क्या योगदान है?
उत्तर:
पारंपरिक ज्ञान जैव विविधता संरक्षण के लिए अनमोल है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और सतत उपयोग पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, आदिवासी समुदायों के पास बहुत पुराना वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण का ज्ञान होता है, जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों, जड़ी-बूटियों, जल स्रोतों के प्रबंधन, और वन्यजीवों के संरक्षण के तरीकों से जुड़ा होता है। यह ज्ञान जैव विविधता को स्थिर बनाए रखने में सहायक है।
123. जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारी कदम क्या हैं?
उत्तर:
भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं:
- राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 – इसके तहत जैव विविधता संरक्षण और इसके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) – यह प्राधिकरण जैव विविधता का संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) – पर्यावरण और जैव विविधता के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा संरक्षण सुनिश्चित करता है।
124. जैव विविधता संरक्षण में आर्थिक दृष्टिकोण क्या है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण में आर्थिक दृष्टिकोण से यह देखा जाता है कि प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता हमारे आर्थिक विकास में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि, औषधि उद्योग, इको-पर्यटन, और जैविक खेती जैव विविधता से संबंधित प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इन संसाधनों का संरक्षण न केवल पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है।
125. जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए क्या वैश्विक प्रयास किए गए हैं?
उत्तर:
वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं:
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD) – इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य (Global Biodiversity Targets) – इन लक्ष्यों में जैव विविधता को संरक्षित करना, जैव संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करना और पर्यावरणीय खतरों को कम करना शामिल है।
- पारिस्थितिकी नेटवर्क और संरक्षित क्षेत्र (Ecological Networks and Protected Areas) – विश्वभर में संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया गया है ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके।
126. जैव विविधता के संदर्भ में “विलुप्त होने का संकट” का क्या अर्थ है?
उत्तर:
विलुप्त होने का संकट वह स्थिति है जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाती है कि उसके प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में रहने का खतरा बढ़ जाता है। यह संकट प्राकृतिक आवासों की हानि, जलवायु परिवर्तन, शिकार, और प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। विलुप्त होने के संकट में रहने वाली प्रजातियाँ जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, और इनके संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं।
127. जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का क्या महत्व है?
उत्तर:
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ उन लाभों को कहा जाता है जो मनुष्य को जैव विविधता से प्राप्त होती हैं, जैसे कि हवा की सफाई, जल की आपूर्ति, खाद्य उत्पादन, और जलवायु नियंत्रण। ये सेवाएँ जैव विविधता के स्थायीत्व के कारण संभव होती हैं, और इनके बिना जीवन असंभव हो सकता है।
128. “इकोलॉजिकल फूटप्रिंट” और जैव विविधता का क्या संबंध है?
उत्तर:
इकोलॉजिकल फूटप्रिंट (Ecological Footprint) यह मापने का एक तरीका है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कितनी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। यह जितना बड़ा होता है, उतनी अधिक जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि अधिक संसाधन उपयोग से प्राकृतिक आवासों का विनाश और प्रदूषण होता है। जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब हमारा इकोलॉजिकल फूटप्रिंट सीमित किया जाए।
129. जैव विविधता संरक्षण में “ग्रीनवाशिंग” का क्या अर्थ है?
उत्तर:
ग्रीनवाशिंग (Greenwashing) एक प्रथा है जिसमें कंपनियाँ पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार होने का दावा करती हैं, जबकि वे असल में जैव विविधता या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। यह उपभोक्ताओं को धोखा देने का एक तरीका होता है, इसलिए जैव विविधता संरक्षण में पारदर्शिता और सच्चाई महत्वपूर्ण है।
130. क्या जैव विविधता का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी है, या इसमें नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है?
उत्तर:
जैव विविधता का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। नागरिकों को इस संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में प्रेरित किया जाता है।
- सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता
- स्थानीय परियोजनाओं में सहभागिता
- प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग
इन पहलुओं के द्वारा नागरिक जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (131-150)
131. जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए “नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया” का क्या महत्व है?
उत्तर:
“नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया” जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र जैविक संसाधनों की रक्षा करते हैं। ये क्षेत्र वन्यजीवों की प्रजातियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है ताकि प्राकृतिक आवासों को संरक्षित किया जा सके।
132. जैव विविधता के संरक्षण के लिए “ग्रीन इन्वेस्टमेंट” का क्या महत्व है?
उत्तर:
“ग्रीन इन्वेस्टमेंट” का मतलब उन परियोजनाओं में निवेश करना है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित और टिकाऊ हों। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में ग्रीन इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य उन आर्थिक गतिविधियों में निवेश करना है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं। इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही, पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखा जाता है।
133. जैव विविधता संरक्षण में “विलुप्त प्रजातियों” का संरक्षण कैसे किया जाता है?
उत्तर:
विलुप्त प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। इन प्रजातियों का संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए कई कदम उठाए जाते हैं:
- संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) में इन प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना।
- संवर्धन और पुनः प्रवेश कार्यक्रम (Breeding and Reintroduction Programs) का संचालन।
- जन जागरूकता और शिक्षा द्वारा इनके संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना।
134. जैव विविधता कानून के तहत “वैज्ञानिक अनुसंधान” का क्या महत्व है?
उत्तर:
वैज्ञानिक अनुसंधान जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह प्रजातियों की संख्या, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के संकटों को समझने में मदद करता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अनुसंधान के माध्यम से यह भी पता चलता है कि कौन सी प्रजातियाँ संकट में हैं और कौन से पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा है। इसके परिणामस्वरूप सही नीति निर्माण और संरक्षण योजनाओं का विकास संभव होता है।
135. जैव विविधता संरक्षण के लिए “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR)” का क्या योगदान है?
उत्तर:
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) का जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। कंपनियाँ अपने कार्यों के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जिम्मेदारी निभाती हैं। CSR के अंतर्गत कंपनियाँ पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश करती हैं, जैसे कि वन पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और जैव विविधता संरक्षण में मदद करना। यह पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक है।
136. जैव विविधता संरक्षण में “संवेदनशील प्रजातियाँ” को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?
उत्तर:
संवेदनशील प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती हैं जो प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से विलुप्त होने की कगार पर होती हैं। इन प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनका अस्तित्व पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संवेदनशील प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाती हैं, और इनकी सुरक्षा से अन्य प्रजातियों की भी रक्षा की जा सकती है।
137. जैव विविधता संरक्षण कानून में “निर्यात और आयात नियंत्रण” का क्या महत्व है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण कानून में “निर्यात और आयात नियंत्रण” का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों का व्यापार पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। जैव विविधता अधिनियम के तहत, जैविक संसाधनों के निर्यात और आयात के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यापार टिकाऊ और पारिस्थितिकी के अनुकूल है।
138. जैव विविधता संरक्षण में “संपत्ति अधिकार” का क्या स्थान है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण में संपत्ति अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्थानीय समुदायों और आदिवासियों के पास पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों पर अधिकार होता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस ज्ञान और संसाधनों के उपयोग का उचित अधिकार देना आवश्यक है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय लोगों को उनके पारंपरिक संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करने का अधिकार मिले।
139. जैव विविधता कानून के तहत “जैव विविधता प्रबंधन समिति” (BMC) की भूमिका क्या है?
उत्तर:
जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन में समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह समिति स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन के लिए योजना बनाती है, संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन करती है, और जैविक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करती है।
140. जैव विविधता के संरक्षण में “जैविक संसाधन” का उपयोग कैसे नियंत्रित किया जाता है?
उत्तर:
जैविक संसाधनों का उपयोग जैव विविधता संरक्षण कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए किसी भी जैविक संसाधन के उपयोग से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करता है कि जैविक संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से हो और इससे जैव विविधता को कोई नुकसान न हो।
141. जैव विविधता संरक्षण में “सार्वजनिक भागीदारी” का क्या महत्व है?
उत्तर:
सार्वजनिक भागीदारी जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करती है और उन्हें संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। जनता की भागीदारी से सामुदायिक प्रयासों को मजबूत किया जाता है, और यह जैव विविधता को बचाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है।
142. जैव विविधता संरक्षण में “वैश्विक सहयोग” का क्या महत्व है?
उत्तर:
वैश्विक सहयोग जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है क्योंकि जैव विविधता की समस्याएँ वैश्विक हैं और इसका संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच सहयोग से जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
143. जैव विविधता संरक्षण में “विविधता का मूल्यांकन” कैसे किया जाता है?
उत्तर:
विविधता का मूल्यांकन जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए किया जाता है। इसमें प्रजातियों की संख्या, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति, और जैविक संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।
144. जैव विविधता संरक्षण में “ऑनलाइन संसाधन” का क्या योगदान है?
उत्तर:
ऑनलाइन संसाधन जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्योंकि वे जानकारी के आदान-प्रदान को तेज और सुलभ बनाते हैं। विभिन्न जैविक प्रजातियों के बारे में ऑनलाइन डेटाबेस और शोध पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाने और वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों को समन्वित करने में मदद मिलती है।
145. जैव विविधता संरक्षण में “मानव और पशु सह-अस्तित्व” का क्या महत्व है?
उत्तर:
मानव और पशु सह-अस्तित्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मनुष्य और वन्यजीव एक साथ रहते हैं, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए पारिस्थितिकी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और अन्य मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, ताकि जानवरों और पौधों के प्राकृतिक आवास सुरक्षित रह सकें।
146. जैव विविधता संरक्षण के लिए “जैविक विविधता समझौतों” का क्या महत्व है?
उत्तर:
जैविक विविधता समझौतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए देशों के बीच सहयोग स्थापित करना है। इन समझौतों के तहत, जैविक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और आर्थिक लाभों का वितरण न्यायसंगत रूप से किया जाता है।
147. जैव विविधता संरक्षण में “संगठनों का सहयोग” कैसे काम करता है?
उत्तर:
संगठनों का सहयोग जैव विविधता संरक्षण में विभिन्न संस्थाओं, NGOs, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच साझेदारी के माध्यम से कार्य करता है। इन संगठनों द्वारा संसाधनों, जानकारी और तकनीकी सहायता का आदान-प्रदान किया जाता है, जिससे जैव विविधता के संरक्षण में सहयोग बढ़ता है।
148. जैव विविधता संरक्षण के लिए “प्राकृतिक संसाधन” का सतत उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाता है?
उत्तर:
प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित किया जाता है ताकि उनकी उपलब्धता भविष्य में भी बनी रहे। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी संसाधन का अत्यधिक उपयोग न हो और उसकी पुन:पूर्ति का समय और प्रक्रिया सही तरीके से हो।
149. जैव विविधता संरक्षण में “संविधान और कानून” का क्या योगदान है?
उत्तर:
संविधान और कानून जैव विविधता संरक्षण में संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत में, संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, और इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम, 2002, जो जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है।
150. जैव विविधता के संरक्षण में “नैतिक जिम्मेदारी” का क्या महत्व है?
उत्तर:
नैतिक जिम्मेदारी का मतलब यह है कि सभी मनुष्यों को जैव विविधता की रक्षा के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण केवल कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में निभाना चाहिए।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (151-170)
151. जैव विविधता संरक्षण में “आर्थिक विकास” और “संरक्षण” के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण में “आर्थिक विकास” और “संरक्षण” के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे संतुलित करने के लिए सतत विकास का सिद्धांत अपनाना आवश्यक है, जहां आर्थिक विकास गतिविधियाँ जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाते हुए संतुलित तरीके से की जाती हैं। इसका उदाहरण उन परियोजनाओं के रूप में देखा जा सकता है जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिर कृषि पद्धतियों, और जैविक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
152. जैव विविधता संरक्षण में “स्थानीय समुदायों” का क्या योगदान है?
उत्तर:
स्थानीय समुदायों का जैव विविधता संरक्षण में अत्यधिक योगदान है, क्योंकि उनके पास पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों का लंबे समय से संरक्षण करने का अनुभव होता है। ये समुदाय प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने में मदद करते हैं। समुदायों को जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रमों में भागीदार बनाने से प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।
153. जैव विविधता संरक्षण के लिए “सरकारों” का क्या रोल है?
उत्तर:
सरकारें जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे नीति निर्माण, कानूनों का कार्यान्वयन, और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। सरकारें जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, और इस क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, सरकारें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता की सुरक्षा के लिए समझौतों और सहयोगों को बढ़ावा देती हैं।
154. जैव विविधता संरक्षण में “मूल्यांकन और निगरानी” का क्या महत्व है?
उत्तर:
मूल्यांकन और निगरानी जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक उपकरण हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि संरक्षण कार्यक्रम प्रभावी हैं और जैविक संसाधन सही तरीके से संरक्षित हो रहे हैं। मूल्यांकन के माध्यम से जैव विविधता की स्थिति का आकलन किया जाता है, जबकि निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि इन प्रयासों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है।
155. जैव विविधता संरक्षण में “विलुप्तप्राय प्रजातियाँ” के पुनर्संस्कार का क्या तरीका है?
उत्तर:
विलुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्संस्कार के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे कि प्रजनन कार्यक्रम (Breeding Programs), प्राकृतिक आवासों का पुनर्निर्माण (Habitat Restoration), और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों (Wildlife Conservation Centers) का निर्माण। इन प्रजातियों का पुनर्संस्कार यह सुनिश्चित करता है कि उनकी संख्या बढ़े और वे प्राकृतिक आवासों में फिर से प्रवृत्त हो सकें।
156. जैव विविधता संरक्षण में “संविधान” की भूमिका क्या है?
उत्तर:
संविधान जैव विविधता संरक्षण में आधारभूत भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A(g) के तहत पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के प्रति राज्य और नागरिकों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।
157. जैव विविधता के संरक्षण में “जन जागरूकता” का क्या महत्व है?
उत्तर:
जन जागरूकता जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को जैव विविधता के महत्व और उसके संरक्षण के उपायों के बारे में शिक्षित करती है। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोग समझते हैं कि उनके कार्य जैव विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं और वे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार बन सकते हैं।
158. जैव विविधता संरक्षण में “आर्थिक रूप से स्थिरता” कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
उत्तर:
आर्थिक रूप से स्थिरता जैव विविधता संरक्षण में “सतत विकास” के सिद्धांत के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें ऐसी नीतियों और योजनाओं को लागू किया जाता है जो पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैविक खेती और पारिस्थितिकी पर्यटन जैसी गतिविधियाँ जैव विविधता का संरक्षण करते हुए स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत बन सकती हैं।
159. जैव विविधता संरक्षण में “वन्यजीव संरक्षण” के लिए कौन से प्रमुख उपाय किए जाते हैं?
उत्तर:
वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रमुख उपाय किए जाते हैं, जैसे:
- संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) की स्थापना।
- वन्यजीव अपराधों पर कड़ी निगरानी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून।
- प्रजनन और पुनः प्रवेश कार्यक्रम (Breeding and Reintroduction Programs)।
- पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ावा देना।
160. जैव विविधता कानून में “आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान” क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर:
आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जब विभिन्न देशों, संगठनों और समुदायों के बीच जैव विविधता से संबंधित जानकारी साझा की जाती है, तो इससे सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों का विकास होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के संरक्षण में तेजी आती है।
161. जैव विविधता संरक्षण में “पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं” का क्या महत्व है?
उत्तर:
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये प्राकृतिक सेवाएँ जैसे जल शोधन, मिट्टी का संरक्षण, और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। इन सेवाओं का संरक्षण जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये मानव जीवन की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
162. जैव विविधता के संरक्षण के लिए “वैज्ञानिक अनुसंधान” का क्या योगदान है?
उत्तर:
वैज्ञानिक अनुसंधान जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह प्रजातियों के जीवन चक्र, उनके आवासों, और उनके संरक्षण के उपायों को समझने में मदद करता है। अनुसंधान के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियाँ और बेहतर संरक्षण रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं, जो जैव विविधता को संरक्षित रखने में सहायक हों।
163. जैव विविधता के संरक्षण में “बायोटेक्नोलॉजी” का क्या योगदान है?
उत्तर:
बायोटेक्नोलॉजी जैव विविधता संरक्षण में नए और बेहतर उपायों के विकास में सहायक हो सकती है। यह तकनीक जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए नए तरीके विकसित करती है, जैसे कि जीन बैंकिंग, पुनःप्रजनन और पौधों तथा जानवरों की प्रजातियों के लिए आनुवंशिक संशोधन।
164. जैव विविधता संरक्षण में “पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली” के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं?
उत्तर:
पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं, जैसे:
- वनों का पुनःरोपण (Reforestation)।
- जल स्रोतों का पुनर्निर्माण (Water Source Restoration)।
- प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और पुनर्निर्माण। इन कदमों से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है।
165. जैव विविधता संरक्षण के लिए “स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण” क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तंत्र स्थानीय प्रजातियों और जैविक संसाधनों के अस्तित्व का आधार हैं। जब इन पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित किया जाता है, तो इससे स्थानीय स्तर पर जैव विविधता बनी रहती है और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में भी मदद मिलती है।
166. जैव विविधता कानून के तहत “उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी” क्या है?
उत्तर:
जैव विविधता कानून के तहत उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी यह है कि वे जैविक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करें, जिससे जैव विविधता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। उपयोगकर्ताओं को जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए।
जैव विविधता संरक्षण कानून (Biodiversity Protection Law) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर (167-180)
167. जैव विविधता संरक्षण में “सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग” कैसे काम करता है?
उत्तर:
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों क्षेत्रों के संसाधनों और क्षमताओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। सरकारें नीतियाँ बनाती हैं और निजी क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के तौर पर, निजी क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश और सरकार के संरक्षण प्रयासों का संयोजन जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। इसके अलावा, कंपनियां पर्यावरणीय जिम्मेदारी के तहत परियोजनाओं में भाग ले सकती हैं।
168. जैव विविधता संरक्षण में “जैविक संसाधनों का व्यापार” कैसे नियंत्रित किया जाता है?
उत्तर:
जैविक संसाधनों का व्यापार जैव विविधता संरक्षण कानूनों के तहत नियंत्रित किया जाता है ताकि इन संसाधनों का अत्यधिक और अवैध शोषण न हो। इसके लिए “नागोया प्रोटोकॉल” और “कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD)” जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत व्यापार पर निगरानी रखी जाती है। व्यापार को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक देश के भीतर नियम और नीतियाँ लागू की जाती हैं, और संसाधनों का व्यापार केवल उन समुदायों और देशों के अधिकारों के तहत किया जाता है जिन्होंने इन संसाधनों का संरक्षण किया है।
169. जैव विविधता संरक्षण के लिए “प्राकृतिक आपदाओं” का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर:
प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा, और तूफान जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। इन आपदाओं से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, जिससे प्रजातियों की विलुप्ति का खतरा बढ़ जाता है। इन घटनाओं के दौरान, जैव विविधता संरक्षण उपायों को पुनर्स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप, प्राकृतिक आपदाओं के बाद पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और नष्ट हुए आवासों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है।
170. जैव विविधता संरक्षण में “जनसंख्या वृद्धि” का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
जनसंख्या वृद्धि जैव विविधता पर दबाव डालती है क्योंकि अधिक जनसंख्या का मतलब है अधिक संसाधनों की खपत, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्रों का नुकसान हो सकता है। अधिक जनसंख्या के कारण वनस्पति और वन्यजीवों के आवासों में कमी होती है, और इससे जैव विविधता में कमी आ सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियोजन, सतत विकास और पर्यावरणीय शिक्षा का प्रचार किया जाता है।
171. जैव विविधता संरक्षण में “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” का क्या महत्व है?
उत्तर:
जैव विविधता संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता सीमाओं से परे होती है, और यह सभी देशों द्वारा साझा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे “कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी” (CBD) और “नागोया प्रोटोकॉल” के तहत देशों को जैव विविधता के संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संरक्षण प्रयासों को साझा किया जाता है, और प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
172. जैव विविधता संरक्षण में “वैश्विक जलवायु परिवर्तन” का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैव विविधता पर गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। बढ़ती गर्मी, समुद्र स्तर का बढ़ना, और बदलते मौसम पैटर्न जैव विविधता के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इससे प्रजातियों का आवास नष्ट हो सकता है या उनका व्यवहार प्रभावित हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और जलवायु अनुकूलन उपायों को लागू करना आवश्यक है।
173. जैव विविधता कानून में “संविधानिक अधिकारों” का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर:
संविधानिक अधिकार जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह अधिकार नागरिकों को पर्यावरणीय न्याय, स्वच्छ हवा, पानी, और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
174. जैव विविधता संरक्षण में “संसारिक दृष्टिकोण” कैसे प्रभावी हो सकता है?
उत्तर:
संसारिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जैव विविधता संरक्षण को केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए। यह दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करता है कि जैव विविधता संरक्षण से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ हो, बल्कि समुदायों को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ पहुंचे। यह दृष्टिकोण जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए अधिक समावेशी और सतत तरीके अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
175. जैव विविधता संरक्षण में “स्थानीय संसाधनों” का क्या योगदान है?
उत्तर:
स्थानीय संसाधन जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं क्योंकि ये संसाधन स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों का हिस्सा होते हैं और इनका संरक्षण पारंपरिक ज्ञान और समुदायों द्वारा किया जाता है। स्थानीय संसाधनों के संरक्षण से जैव विविधता बनी रहती है, और समुदायों को इन संसाधनों से आय का स्रोत भी मिलता है।
176. जैव विविधता संरक्षण में “प्राकृतिक पूंजी” की अवधारणा का क्या महत्व है?
उत्तर:
प्राकृतिक पूंजी का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य समझा जाता है और यह संकेत मिलता है कि इनका संरक्षण आर्थिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण करने से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
177. जैव विविधता संरक्षण में “संवेदनशील प्रजातियों” का संरक्षण कैसे किया जाता है?
उत्तर:
संवेदनशील प्रजातियों का संरक्षण विशिष्ट उपायों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि उनका आवास संरक्षित करना, प्रजनन कार्यक्रमों का संचालन, और जंगली क्षेत्र के लिए संरक्षण योजना बनाना। इसके अलावा, इन प्रजातियों की निगरानी करना और उन पर अवैध शिकार तथा शिकार के प्रयासों को रोकना आवश्यक है।
178. जैव विविधता संरक्षण में “जैविक संसाधनों का प्रबंधन” कैसे किया जाता है?
उत्तर:
जैविक संसाधनों का प्रबंधन सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहें। यह प्रबंधन वैज्ञानिक अनुसंधान, पारंपरिक ज्ञान, और समुदाय आधारित प्रबंधन रणनीतियों के संयोजन से किया जाता है, ताकि संसाधनों का अधिकतम और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके।
179. जैव विविधता संरक्षण में “कानूनी ढांचा” कितना प्रभावी है?
उत्तर:
कानूनी ढांचा जैव विविधता संरक्षण में अत्यधिक प्रभावी होता है क्योंकि यह संरक्षण प्रयासों को कानूनी वैधता प्रदान करता है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करता है। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए कानून जैव विविधता के संरक्षण के लिए निर्देशों, प्रतिबंधों और प्रोत्साहनों का निर्धारण करते हैं। इन कानूनों के तहत नागरिकों और संगठनों को जैव विविधता संरक्षण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
180. जैव विविधता संरक्षण में “पर्यावरणीय न्याय” का क्या महत्व है?
उत्तर:
पर्यावरणीय न्याय जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो और समाज के सभी वर्गों को इन संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो। यह सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों को जैव विविधता से संबंधित नुकसान से बचाया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।
निष्कर्ष:
भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई कानूनी और नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम, 2002 इसका प्रमुख कानून है, जो जैव संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। नागरिकों की भागीदारी और कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ ही जैव विविधता का प्रभावी संरक्षण संभव है।