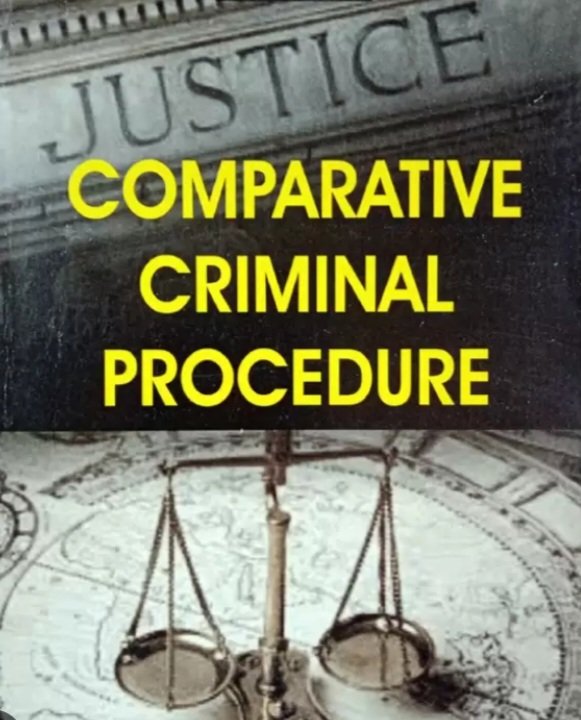Comparative Criminal Procedure (तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) विभिन्न देशों में लागू आपराधिक न्याय प्रणालियों (Criminal Justice Systems) की तुलना और अध्ययन से संबंधित विषय है। इसमें मुख्य रूप से अभियोजन प्रणाली (Prosecution System), पुलिस शक्तियाँ (Police Powers), न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process), और न्यायालयों की संरचना (Structure of Courts) की तुलना की जाती है।
नीचे इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं:
प्रश्न 1: तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) क्या है?
उत्तर:
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया एक अध्ययन है जिसमें विभिन्न देशों में लागू आपराधिक कानूनों और प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है। यह न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता, अभियोजन प्रक्रिया, बचाव प्रक्रिया, पुलिस शक्तियों, और न्यायिक समीक्षा पर केंद्रित होता है।
प्रश्न 2: आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख मॉडल कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
आपराधिक न्याय प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रमुख मॉडलों में विभाजित की जाती है:
- अभियोगात्मक प्रणाली (Adversarial System)
- यह प्रणाली मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, और भारत जैसे देशों में अपनाई जाती है।
- इसमें अभियोजन पक्ष (Prosecution) और बचाव पक्ष (Defense) के बीच मुकदमेबाजी होती है।
- न्यायाधीश एक तटस्थ मध्यस्थ (Neutral Arbitrator) की भूमिका निभाते हैं।
- इनक्विजिटोरियल प्रणाली (Inquisitorial System)
- यह प्रणाली मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी, और अन्य यूरोपीय देशों में अपनाई जाती है।
- न्यायाधीश मामले की जाँच में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- अभियोजन और बचाव की प्रक्रिया न्यायालय के अधीन होती है।
प्रश्न 3: भारत और अमेरिका की आपराधिक प्रक्रिया में क्या प्रमुख अंतर हैं?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका |
|——-|——|——–|
| न्याय प्रणाली | अभियोगात्मक (Adversarial) | अभियोगात्मक (Adversarial) |
| संविधान का प्रभाव | भारतीय संविधान, IPC, CrPC | अमेरिकी संविधान, Bill of Rights |
| पुलिस शक्तियाँ | गिरफ्तारी और जाँच के लिए न्यायिक अनुमति आवश्यक | पुलिस को अधिक स्वायत्तता |
| जूरी प्रणाली | जूरी प्रणाली नहीं | जूरी प्रणाली प्रमुख |
| मृत्युदंड | दिया जाता है, लेकिन दुर्लभतम मामलों में | कुछ राज्यों में निषेध, कुछ में लागू |
प्रश्न 4: अभियोजन (Prosecution) की प्रक्रिया भारत और ब्रिटेन में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: अभियोजन प्रक्रिया मुख्य रूप से सरकारी अभियोजकों (Public Prosecutors) द्वारा चलाई जाती है, और वे स्वतंत्र होते हैं।
- ब्रिटेन: अभियोजन का कार्य “क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS)” द्वारा किया जाता है, जो अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करता है और पुलिस से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
प्रश्न 5: जूरी प्रणाली (Jury System) क्या होती है और यह किन देशों में लागू है?
उत्तर:
जूरी प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसमें आम नागरिकों का एक समूह (जूरी) किसी मामले में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेता है।
- अमेरिका, ब्रिटेन, और कनाडा जैसे देशों में जूरी प्रणाली प्रभावी रूप से लागू है।
- भारत और कई अन्य एशियाई देशों में यह प्रणाली नहीं अपनाई गई है।
प्रश्न 6: भारत में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) और पुलिस हिरासत (Police Custody) में क्या अंतर है?
उत्तर:
| पहलू | पुलिस हिरासत | न्यायिक हिरासत |
|———|————–|—————-|
| निगरानी | पुलिस द्वारा | न्यायालय के आदेश से |
| अवधि | 24 घंटे से अधिक नहीं (मजिस्ट्रेट की अनुमति से 15 दिन तक) | 90 दिन तक (गंभीर मामलों में) |
| उद्देश्य | जाँच के लिए | आरोपी को जेल में रखना |
प्रश्न 7: Habeas Corpus (हैबियस कॉर्पस) याचिका क्या होती है?
उत्तर:
Habeas Corpus एक संवैधानिक अधिकार है, जिसका उपयोग अवैध हिरासत (Illegal Detention) के खिलाफ किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, तो वह या उसका प्रतिनिधि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल कर सकते हैं।
प्रश्न 8: अमेरिका में ‘Miranda Rights’ क्या होते हैं?
उत्तर:
अमेरिका में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा “Miranda Warning” दिया जाता है, जिसमें उसके अधिकार बताए जाते हैं:
- चुप रहने का अधिकार (Right to remain silent)
- वकील पाने का अधिकार (Right to an attorney)
- पुलिस पूछताछ में जवाब न देने का अधिकार
यदि पुलिस ने यह चेतावनी नहीं दी, तो आरोपी के बयान अदालत में अमान्य हो सकते हैं।
प्रश्न 9: भारत में आपराधिक न्याय सुधारों (Criminal Justice Reforms) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- मालिमथ कमेटी (Malimath Committee) ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश की, जैसे:
- पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली
- पुलिस सुधार
- अभियोजन प्रक्रिया में सुधार
- हाल के वर्षों में भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।
प्रश्न 10: निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तर:
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न देशों की न्याय प्रणालियों की ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। इससे न्याय प्रणाली में सुधार लाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं।
यहाँ और महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) को और गहराई से समझने में मदद करेंगे।
प्रश्न 11: भारत और फ्रांस की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या अंतर है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | फ्रांस |
|———|———|——–|
| न्याय प्रणाली | अभियोगात्मक (Adversarial) | इनक्विजिटोरियल (Inquisitorial) |
| न्यायाधीश की भूमिका | निष्पक्ष मध्यस्थ | जाँच प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार |
| पुलिस जाँच | पुलिस स्वतंत्र रूप से जाँच करती है | न्यायाधीश (Investigating Judge) जांच को नियंत्रित करता है |
| अदालतों का ढांचा | सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतें | Cassation Court (सर्वोच्च), Appellate Courts, Trial Courts |
प्रश्न 12: आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) किन देशों में अधिक और किनमें कम है?
उत्तर:
- जापान: दोषसिद्धि दर सबसे अधिक (99%) होती है क्योंकि वहाँ अभियोजन पक्ष केवल मजबूत मामलों को ही अदालत में ले जाता है।
- अमेरिका: दोषसिद्धि दर 85-90% है, लेकिन Plea Bargaining (सौदेबाजी) आम है।
- भारत: दोषसिद्धि दर अपेक्षाकृत कम (~50%) है, क्योंकि कई मामलों में साक्ष्य और जाँच की कमजोरी होती है।
प्रश्न 13: Plea Bargaining (दोषी ठहरने का समझौता) क्या होता है और यह किन देशों में लागू है?
उत्तर:
- परिभाषा: Plea Bargaining वह प्रक्रिया है जिसमें आरोपी अदालत के सामने कुछ शर्तों के तहत खुद को दोषी मान लेता है और बदले में उसे कम सजा मिलती है।
- अमेरिका: व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, अधिकांश आपराधिक मामलों का निपटारा इसी से होता है।
- भारत: सीमित मामलों में लागू (CrPC की धारा 265A-265L के तहत केवल कम गंभीर अपराधों में मान्य)।
- यूरोप: फ्रांस और जर्मनी में कुछ हद तक प्रयोग किया जाता है, लेकिन न्यायाधीश इसकी समीक्षा करते हैं।
प्रश्न 14: ‘Double Jeopardy’ (दोहरे मुकदमे से संरक्षण) का सिद्धांत क्या है?
उत्तर:
- यह सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- भारत में: अनुच्छेद 20(2) के तहत संरक्षित।
- अमेरिका में: पाँचवें संशोधन (Fifth Amendment) के तहत यह अधिकार दिया गया है।
- यूरोप में: अधिकांश देशों में इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन अपील और पुनर्विचार अपवाद हो सकते हैं।
प्रश्न 15: क्या अमेरिका में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार है?
उत्तर:
हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ:
- Felony (गंभीर अपराध) मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है।
- Misdemeanor (छोटे अपराध) के लिए आमतौर पर वारंट आवश्यक होता है, जब तक कि अपराध पुलिस के सामने न हुआ हो।
- Exigent Circumstances (विशेष परिस्थितियाँ) जैसे कि जब कोई अपराध तुरंत रोका जाना जरूरी हो, पुलिस बिना वारंट के कार्य कर सकती है।
प्रश्न 16: भारत और जर्मनी की आपराधिक प्रक्रिया में क्या अंतर हैं?
उत्तर:
| तत्व | भारत | जर्मनी |
|———|———|———|
| न्याय प्रणाली | अभियोगात्मक (Adversarial) | इनक्विजिटोरियल (Inquisitorial) |
| न्यायाधीश की भूमिका | निष्पक्ष मध्यस्थ | सक्रिय जाँचकर्ता |
| अभियोजन प्रणाली | सरकारी अभियोजक स्वतंत्र होते हैं | अभियोजन न्यायपालिका के अधीन होता है |
| साक्ष्य संग्रहण | पुलिस स्वतंत्र रूप से साक्ष्य एकत्र करती है | न्यायाधीश द्वारा निगरानी होती है |
प्रश्न 17: ‘Mens Rea’ और ‘Actus Reus’ का क्या अर्थ है?
उत्तर:
- Mens Rea (अपराध करने की मंशा) – अपराध करने की मानसिक स्थिति या इरादा।
- Actus Reus (अवैध कृत्य) – वह वास्तविक अवैध कार्य जो किया गया है।
- अपराध सिद्ध होने के लिए दोनों आवश्यक होते हैं, सिवाय स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी (Strict Liability) अपराधों के।
प्रश्न 18: ‘Right to Fair Trial’ किन देशों में कैसे लागू है?
उत्तर:
- भारत: अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
- अमेरिका: छठा संशोधन (Sixth Amendment) अपराधी को निष्पक्ष सुनवाई और वकील का अधिकार देता है।
- यूरोप: यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स (ECHR) निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है।
प्रश्न 19: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) क्या है?
उत्तर:
- स्थापना: 2002 में “रोम संधि” (Rome Statute) के तहत।
- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।
- कार्य: युद्ध अपराध, नरसंहार (Genocide), मानवता के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाना।
- भारत और अमेरिका की स्थिति: भारत और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं हैं।
प्रश्न 20: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न देशों की न्यायिक प्रणालियों की समझ को बेहतर बनाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग देश अपनी कानूनी व्यवस्था को अपनी सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर विकसित करते हैं।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी या सामान्य ज्ञान बढ़ाने में मदद करेंगे।
प्रश्न 21: ‘Bail’ (जमानत) की प्रक्रिया भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका | ब्रिटेन |
|———|———|———|———|
| जमानत के प्रकार | जमानतीय और गैर-जमानतीय अपराध | व्यक्तिगत जमानत, नकद जमानत | समान्य जमानत, सशर्त जमानत |
| अधिकार | जमानत संवैधानिक अधिकार नहीं | 8वें संशोधन में जमानत का उल्लेख | जमानत कानून ‘Bail Act, 1976’ द्वारा नियंत्रित |
| न्यायालय का विवेकाधिकार | न्यायालय अपराध की प्रकृति के आधार पर निर्णय लेता है | अभियुक्त की पिछली अपराध-रिकॉर्ड देखी जाती है | अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए |
प्रश्न 22: अमेरिका और भारत में मृत्युदंड (Capital Punishment) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत: दुर्लभतम मामलों (Rarest of the rare) में मृत्युदंड दिया जाता है।
- अमेरिका: कुछ राज्यों में मृत्युदंड लागू है, कुछ राज्यों में इसे समाप्त कर दिया गया है।
- मुख्य अंतर:
- भारत में फांसी (Hanging) का प्रयोग होता है, जबकि अमेरिका में Lethal Injection, Electric Chair, और Firing Squad जैसी विधियाँ अपनाई जाती हैं।
प्रश्न 23: आपराधिक मामलों में अपील की प्रक्रिया भारत, अमेरिका और फ्रांस में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका | फ्रांस |
|———|———|———|———|
| अपील का अधिकार | हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार | संघीय (Federal) और राज्य (State) स्तर पर अपील | Cassation Court (सर्वोच्च न्यायालय) अंतिम अपील सुनता है |
| रिव्यू और पुनर्विचार याचिका | पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है | सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला नहीं जा सकता | समीक्षा न्यायालय द्वारा सीमित दायरे में होती है |
प्रश्न 24: ‘Police Interrogation’ (पुलिस पूछताछ) के अधिकार भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत:
- आरोपी चुप रहने का अधिकार रखता है (Article 20(3), भारतीय संविधान)।
- पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
- अमेरिका:
- आरोपी को Miranda Warning दी जाती है (Miranda v. Arizona केस)।
- बिना वकील की अनुमति के पुलिस गहन पूछताछ नहीं कर सकती।
प्रश्न 25: साक्ष्य कानून (Law of Evidence) भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका | ब्रिटेन |
|———|———|———|———|
| प्रमुख कानून | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | Federal Rules of Evidence | Criminal Evidence Act, 1898 |
| गोपनीयता (Privilege) | पति-पत्नी के बीच बातचीत साक्ष्य नहीं बन सकती | वकील-मुवक्किल गोपनीयता मजबूत | न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर |
| गैर-स्वीकार्य साक्ष्य | अवैध तरीके से प्राप्त साक्ष्य अमान्य हो सकते हैं | अवैध साक्ष्य अमान्य हो सकते हैं (Exclusionary Rule) | न्यायालय को विवेक का अधिकार |
प्रश्न 26: मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कौन-कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते और संस्थाएँ कार्यरत हैं?
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) – मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निगरानी।
- यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) – यूरोप में मानवाधिकार संबंधी मामलों की सुनवाई करता है।
- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) – युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाता है।
- जेनेवा संधियाँ (Geneva Conventions) – युद्धकाल में मानवाधिकारों की रक्षा।
प्रश्न 27: भारत में पुलिस हिरासत (Police Custody) और न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के बीच अंतर क्या है?
उत्तर:
| तत्व | पुलिस हिरासत | न्यायिक हिरासत |
|———|————–|—————-|
| निगरानी | पुलिस द्वारा | न्यायालय के आदेश से |
| अवधि | 15 दिन तक (मजिस्ट्रेट की अनुमति से) | 90 दिन तक (गंभीर मामलों में) |
| उद्देश्य | पूछताछ और जाँच के लिए | आरोपी को जेल में रखना |
प्रश्न 28: कौन-कौन से अपराध “Strict Liability Crimes” की श्रेणी में आते हैं?
उत्तर:
- Strict Liability Crimes वे अपराध हैं जिनमें अपराधी की मानसिक स्थिति (Mens Rea) का महत्व नहीं होता, केवल अपराध घटित होना ही पर्याप्त होता है।
- उदाहरण:
- यातायात अपराध (Traffic Violations)
- पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन
- खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपराध
प्रश्न 29: किस प्रकार के अपराधों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर:
- युद्ध अपराध (War Crimes) – युद्ध में नागरिकों पर हमले।
- नरसंहार (Genocide) – जातीय या धार्मिक समूहों का संहार।
- मानवता के खिलाफ अपराध (Crimes Against Humanity) – बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन।
प्रश्न 30: तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन का क्या महत्व है?
उत्तर:
- बेहतर न्याय प्रणाली: विभिन्न देशों की प्रक्रियाओं की तुलना कर सुधार लागू किए जा सकते हैं।
- मानवाधिकारों की रक्षा: नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने में मदद करता है।
- न्याय प्रणाली में पारदर्शिता: विभिन्न न्याय प्रणालियों से सीखकर न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष:
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) का अध्ययन विभिन्न देशों की न्यायिक प्रणालियों को समझने और सुधारने के लिए आवश्यक है। यह कानून के छात्रों, न्यायिक परीक्षा के अभ्यर्थियों और कानूनी शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपके अध्ययन और परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे।
प्रश्न 31: भारत और जर्मनी में अभियोजन (Prosecution) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | जर्मनी |
|———|———|———|
| अभियोजन एजेंसी | सरकारी अभियोजक (Public Prosecutor) | Staatsanwaltschaft (State Prosecution) |
| स्वतंत्रता | अभियोजन स्वतंत्र होता है | अभियोजन न्यायपालिका के अधीन होता है |
| भूमिका | अभियोजक अदालत में आरोप साबित करने का कार्य करता है | अभियोजक निष्पक्ष जांच में शामिल होता है |
प्रश्न 32: क्या अमेरिका में “Right to Remain Silent” (चुप रहने का अधिकार) भारतीय प्रणाली से अलग है?
उत्तर:
- अमेरिका: Miranda Rights के तहत पुलिस को गिरफ्तारी के समय बताना पड़ता है कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है।
- भारत: अनुच्छेद 20(3) के तहत “Self-incrimination” से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन पुलिस को Miranda Warning जैसी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती।
प्रश्न 33: “Habeas Corpus” का क्या महत्व है और यह किन देशों में लागू होता है?
उत्तर:
- यह एक कानूनी सिद्धांत है जो अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारत: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है।
- अमेरिका: संविधान में Habeas Corpus को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ब्रिटेन: Habeas Corpus Act, 1679 के तहत यह अधिकार दिया गया है।
प्रश्न 34: भारत और चीन की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या प्रमुख अंतर हैं?
उत्तर:
| तत्व | भारत | चीन |
|———|———|———|
| न्याय प्रणाली | Adversarial (प्रतिस्पर्धात्मक) | Inquisitorial (अन्वेषणात्मक) |
| न्यायाधीश की भूमिका | निष्पक्ष मध्यस्थ | सक्रिय जांचकर्ता |
| अधिकार संरचना | स्वतंत्र न्यायपालिका | न्यायपालिका सरकार के नियंत्रण में |
| दोषसिद्धि दर | ~50% | ~99% (सरकार का मजबूत नियंत्रण) |
प्रश्न 35: “Plea Bargaining” (दोषी ठहरने का समझौता) भारत और ब्रिटेन में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: सीमित मामलों में (CrPC 265A-265L के तहत) लागू, केवल हल्के अपराधों के लिए।
- ब्रिटेन: अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच अधिक स्वतंत्रता होती है, और न्यायालय इसकी समीक्षा करता है।
प्रश्न 36: क्या किसी देश में जूरी प्रणाली (Jury System) अब भी मौजूद है?
उत्तर:
- अमेरिका: अब भी जूरी प्रणाली लागू है, विशेषकर गंभीर आपराधिक मामलों में।
- भारत: 1959 में इसे समाप्त कर दिया गया (KM Nanavati Case के बाद)।
- ब्रिटेन: अब भी कुछ आपराधिक मामलों में जूरी का प्रयोग होता है।
प्रश्न 37: भारत, अमेरिका और फ्रांस में जमानत प्रणाली में क्या अंतर है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका | फ्रांस |
|———|———|———|———|
| साधारण जमानत | मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है | Bail Bond सिस्टम प्रचलित | न्यायिक नियंत्रण में |
| गंभीर अपराधों में जमानत | कोर्ट के विवेक पर | Bail Hearing अनिवार्य | जमानत सख्त शर्तों के साथ दी जाती है |
| बिना जमानत रिहाई | कुछ मामलों में Police Bail संभव | Personal Recognizance Bond का प्रावधान | Juge d’instruction (न्यायाधीश) तय करता है |
प्रश्न 38: “Double Jeopardy” सिद्धांत भारत और अमेरिका में कैसे लागू होता है?
उत्तर:
- भारत: अनुच्छेद 20(2) के तहत, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं पा सकता।
- अमेरिका: पाँचवें संशोधन के तहत सुरक्षा, लेकिन अपील और कुछ विशेष परिस्थितियों में पुन: मुकदमा संभव है।
प्रश्न 39: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध रोकने के लिए कौन-कौन से संगठन कार्यरत हैं?
उत्तर:
- INTERPOL: अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी।
- Europol: यूरोपीय संघ के भीतर अपराध रोकने के लिए।
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): नशीले पदार्थों और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए।
प्रश्न 40: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न देशों की न्याय प्रणाली की विशेषताओं और अंतर को समझने में मदद करता है। यह वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी और विषय की गहरी समझ में मदद करेंगे।
प्रश्न 41: क्या भारत और अमेरिका में “Pre-trial Detention” (पूर्व-ट्रायल हिरासत) की प्रक्रिया समान है?
उत्तर:
- भारत:
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य (CrPC धारा 57)।
- गैर-जमानती अपराधों में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 90 दिनों तक हो सकती है।
- अमेरिका:
- “Probable Cause” सिद्ध होने पर ही व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है।
- जमानत पर रिहाई संभव, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में हिरासत बढ़ाई जा सकती है।
प्रश्न 42: भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में “Rights of the Accused” (अभियुक्त के अधिकार) में क्या अंतर है?
उत्तर:
| अधिकार | भारत | अमेरिका | ब्रिटेन |
|———–|———|———|———|
| वकील का अधिकार | मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 22) | छठा संशोधन (Sixth Amendment) | वकील का अधिकार सुरक्षित |
| चुप रहने का अधिकार | अनुच्छेद 20(3) | Miranda Warning | कानून के तहत सुरक्षा |
| निष्पक्ष सुनवाई | अनुच्छेद 21 | निष्पक्ष जूरी ट्रायल | निष्पक्ष ट्रायल की गारंटी |
प्रश्न 43: “Trial in Absentia” (गैर-मौजूदगी में मुकदमा) किन देशों में लागू होता है?
उत्तर:
- भारत: दुर्लभ मामलों में ही संभव, लेकिन आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार रहता है।
- फ्रांस: कुछ आपराधिक मामलों में गैर-मौजूदगी में ट्रायल संभव।
- अमेरिका: सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है, जब तक आरोपी जानबूझकर अनुपस्थित न हो।
प्रश्न 44: “Plea of Insanity” (पागलपन की दलील) का सिद्धांत किन देशों में लागू होता है?
उत्तर:
- भारत: IPC की धारा 84 के तहत, यदि आरोपी अपराध करते समय मानसिक रूप से अक्षम था, तो उसे दोषमुक्त किया जा सकता है।
- अमेरिका: M’Naghten Rule और Durham Rule के आधार पर रक्षा की जा सकती है।
- ब्रिटेन: मानसिक विकृति (Mental Disorder Defence) कानूनों के तहत यह लागू होता है।
प्रश्न 45: “Extradition Treaty” (प्रत्यर्पण संधि) क्या है और भारत किन देशों के साथ संधियाँ रखता है?
उत्तर:
- परिभाषा: यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश दूसरे देश को अपराधी सौंपता है।
- भारत के प्रमुख प्रत्यर्पण समझौते: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, UAE, रूस आदि के साथ।
प्रश्न 46: “White Collar Crimes” (सफेदपोश अपराध) से निपटने की प्रक्रिया भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing), ED (Enforcement Directorate) जांच करता है।
- अमेरिका: FBI और SEC (Securities and Exchange Commission) इन अपराधों की जांच करते हैं।
प्रश्न 47: “Cyber Crime Laws” (साइबर अपराध कानून) भारत, अमेरिका और चीन में कैसे अलग हैं?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका | चीन |
|———|———|———|———|
| प्रमुख कानून | IT Act, 2000 | Computer Fraud and Abuse Act | साइबर सुरक्षा कानून |
| सेंसरशिप | कम | आंशिक | सख्त नियंत्रण |
| दंड प्रक्रिया | सजा और जुर्माने का प्रावधान | कड़ी सजा | सरकार की अनुमति से मुकदमा |
प्रश्न 48: भारत और अमेरिका में “Juvenile Justice” (बाल न्याय) प्रणाली में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- 16-18 वर्ष के किशोरों को गंभीर अपराधों में वयस्कों की तरह आज़माया जा सकता है (Juvenile Justice Act, 2015)।
- अमेरिका:
- कुछ राज्यों में 14 साल से ऊपर के बच्चों को वयस्क न्यायालय में भेजा जा सकता है।
प्रश्न 49: भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में पुलिस की शक्तियाँ कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
| पुलिस अधिकार | भारत | अमेरिका | ब्रिटेन |
|————–|———|———|———|
| गिरफ्तारी | वारंट आवश्यक (कुछ मामलों में नहीं) | बिना वारंट गिरफ्तारी संभव | PACE Act, 1984 के तहत सीमित अधिकार |
| हथियारों का उपयोग | सीमित | अधिक स्वतंत्रता | पुलिस आमतौर पर हथियार नहीं रखती |
प्रश्न 50: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन विभिन्न देशों की आपराधिक न्याय प्रणाली की समझ विकसित करने में मदद करता है। यह कानूनी सुधारों और न्यायिक कुशलता बढ़ाने में सहायक होता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 51: “Adversarial” और “Inquisitorial” आपराधिक न्याय प्रणालियों में क्या अंतर है?
उत्तर:
| तत्व | Adversarial प्रणाली | Inquisitorial प्रणाली |
|———|—————–|—————-|
| देश | भारत, अमेरिका, ब्रिटेन | फ्रांस, जर्मनी, चीन |
| न्यायाधीश की भूमिका | मध्यस्थ (Neutral Arbiter) | सक्रिय जांचकर्ता |
| अभियोजन प्रक्रिया | अभियोजन और बचाव पक्ष की प्रतिस्पर्धा | न्यायाधीश साक्ष्य इकट्ठा करता है |
| साक्ष्य कानून | कठोर नियम | अधिक लचीला |
प्रश्न 52: क्या “Right to Speedy Trial” (शीघ्र न्याय का अधिकार) सभी देशों में समान है?
उत्तर:
- भारत: अनुच्छेद 21 के तहत यह मौलिक अधिकार है।
- अमेरिका: छठा संशोधन “Speedy Trial Act, 1974” लागू करता है।
- ब्रिटेन: न्यायालय उचित समय सीमा में ट्रायल सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 53: भारत और अमेरिका में “Plea Bargaining” (दोषसवीकार समझौता) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- CrPC की धारा 265A-265L के तहत सीमित अपराधों में लागू।
- गंभीर अपराधों में अनुमति नहीं है।
- अमेरिका:
- अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच अधिक स्वतंत्रता।
- न्यायालय केवल सहमति की समीक्षा करता है।
प्रश्न 54: “Right Against Self-Incrimination” (स्वयं के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार) भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: अनुच्छेद 20(3) के तहत सुरक्षा, आरोपी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता।
- अमेरिका: पाँचवाँ संशोधन (“Taking the Fifth”) आरोपी को यह अधिकार देता है।
प्रश्न 55: आपराधिक मामलों में “Legal Aid” (निःशुल्क कानूनी सहायता) किन देशों में लागू है?
उत्तर:
- भारत: संविधान के अनुच्छेद 39A और “Legal Services Authorities Act, 1987” के तहत।
- अमेरिका: “Gideon v. Wainwright (1963)” के बाद सार्वजनिक बचाव वकील की व्यवस्था।
- ब्रिटेन: “Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act, 2012” लागू।
प्रश्न 56: “Forensic Evidence” (न्यायिक साक्ष्य) भारत और अन्य देशों में कैसे स्वीकार्य होता है?
उत्तर:
- भारत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकार्य।
- अमेरिका: “Daubert Standard” लागू, वैज्ञानिक प्रमाणिकता आवश्यक।
- ब्रिटेन: न्यायालय न्यायिक विवेक पर निर्णय लेता है।
प्रश्न 57: “Rights of Victims” (पीड़ितों के अधिकार) भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत: पीड़ित मुआवजा योजना (Victim Compensation Scheme) लागू।
- अमेरिका: “Victims’ Rights and Restitution Act, 1990” लागू।
प्रश्न 58: भारत, अमेरिका और जापान में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
| देश | मृत्युदंड की स्थिति |
|——–|—————–|
| भारत | दुर्लभतम मामलों में (Rarest of the Rare) |
| अमेरिका | कुछ राज्यों में लागू, कुछ में प्रतिबंधित |
| जापान | गंभीर अपराधों में अब भी दी जाती है |
प्रश्न 59: “Hate Crimes” (घृणा अपराध) से निपटने के लिए विभिन्न देशों में क्या कानून हैं?
उत्तर:
- भारत: IPC की धारा 153A, 295A घृणा फैलाने वाले अपराधों पर रोक लगाती है।
- अमेरिका: “Hate Crimes Prevention Act, 2009” लागू।
- ब्रिटेन: “Public Order Act, 1986” घृणास्पद भाषणों पर प्रतिबंध लगाता है।
प्रश्न 60: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन न्यायिक सुधारों को समझने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 61: भारत और जर्मनी में “Preventive Detention” (निवारक निरोध) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत: संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत 3 महीने तक निवारक हिरासत संभव है, इसके बाद सलाहकार बोर्ड की अनुमति आवश्यक है।
- जर्मनी: बिना न्यायिक समीक्षा के लंबे समय तक हिरासत संभव नहीं होती।
प्रश्न 62: “Contempt of Court” (न्यायालय की अवमानना) कानून भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत:
- “Contempt of Courts Act, 1971” लागू।
- न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सख्त दंड।
- अमेरिका:
- “Freedom of Speech” (पहला संशोधन) के कारण अवमानना कानून अपेक्षाकृत उदार।
प्रश्न 63: भारत और ब्रिटेन में “Police Custody” और “Judicial Custody” में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- पुलिस हिरासत अधिकतम 15 दिन (CrPC धारा 167)।
- न्यायिक हिरासत 90 दिनों तक बढ़ सकती है।
- ब्रिटेन:
- पुलिस हिरासत अधिकतम 96 घंटे (PACE Act, 1984)।
- जमानत या न्यायिक हिरासत का निर्णय मजिस्ट्रेट करता है।
प्रश्न 64: भारत, अमेरिका और फ्रांस में “Double Jeopardy” सिद्धांत कैसे लागू होता है?
उत्तर:
| देश | Double Jeopardy का प्रावधान |
|——–|—————-|
| भारत | अनुच्छेद 20(2) – एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं। |
| अमेरिका | पाँचवें संशोधन में सुरक्षा, कुछ अपवाद संभव। |
| फ्रांस | Double Jeopardy की सीमित स्वीकार्यता। |
प्रश्न 65: “Solitary Confinement” (एकांत कारावास) भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: केवल दुर्लभ मामलों में IPC धारा 73-74 के तहत।
- अमेरिका: कुछ राज्यों में लंबे समय तक एकांत कारावास विवादास्पद है।
प्रश्न 66: भारत, अमेरिका और चीन में “Bail System” (जमानत प्रणाली) में क्या अंतर है?
उत्तर:
| देश | जमानत प्रणाली |
|——–|—————-|
| भारत | जमानत मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर। |
| अमेरिका | Bail Bondsmen द्वारा जमानत प्रक्रिया संभव। |
| चीन | जमानत दुर्लभ, अधिक सरकारी नियंत्रण। |
प्रश्न 67: भारत और रूस में “Criminal Appeal System” (आपराधिक अपील प्रणाली) में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत: जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय।
- रूस: तीन-स्तरीय अपीलीय प्रणाली, कुछ मामलों में पुनरीक्षण (Cassation)।
प्रश्न 68: “Eyewitness Testimony” (प्रत्यक्षदर्शी गवाही) भारत और अमेरिका में कितनी विश्वसनीय मानी जाती है?
उत्तर:
- भारत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकार्य, लेकिन न्यायिक सतर्कता आवश्यक।
- अमेरिका: वैज्ञानिक शोधों के कारण इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं, क्रॉस-एग्जामिनेशन आवश्यक।
प्रश्न 69: भारत, अमेरिका और जापान में “Confession” (स्वीकृति) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
| देश | स्वीकृति का नियम |
|——–|—————-|
| भारत | पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अदालत में मान्य नहीं (धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम)। |
| अमेरिका | Miranda Rights के तहत चेतावनी देना आवश्यक। |
| जापान | पुलिस दबाव में लिए गए बयानों को मान्यता मिल सकती है। |
प्रश्न 70: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन विभिन्न देशों की न्याय प्रणाली को बेहतर समझने और सुधार की दिशा में कार्य करने में सहायक होता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 71: भारत और अमेरिका में “Hearsay Evidence” (अफवाह या सुनी-सुनाई गवाही) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 के तहत “Hearsay Evidence” आमतौर पर अस्वीकार्य होती है।
- कुछ अपवाद हैं, जैसे “Dying Declaration” (मृत्यु पूर्व कथन)।
- अमेरिका:
- “Federal Rules of Evidence” में “Hearsay Rule” लागू है।
- कुछ अपवादों के तहत मान्य हो सकता है, जैसे “Excited Utterance” और “Business Records Exception”।
प्रश्न 72: भारत और ब्रिटेन में “Judicial Review” (न्यायिक समीक्षा) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार।
- सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास विधायी और कार्यकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति।
- ब्रिटेन:
- न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश क्योंकि संसद सर्वोच्च है।
- केवल प्रशासनिक फैसलों की वैधता पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
प्रश्न 73: भारत, अमेरिका और फ्रांस में “Burden of Proof” (साक्ष्य का भार) कैसे निर्धारित होता है?
उत्तर:
| देश | साक्ष्य का भार |
|——–|—————-|
| भारत | अभियोजन पक्ष पर (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101)। |
| अमेरिका | “Beyond a Reasonable Doubt” मानक अपनाया जाता है। |
| फ्रांस | जज की जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। |
प्रश्न 74: भारत और चीन में “Surveillance Laws” (निगरानी कानून) की तुलना कीजिए।
उत्तर:
- भारत:
- “Information Technology Act, 2000” और “Indian Telegraph Act, 1885” के तहत सरकारी निगरानी संभव।
- निगरानी के लिए कानूनी प्रक्रिया आवश्यक।
- चीन:
- सरकार का कड़ा नियंत्रण, “Cybersecurity Law, 2017” लागू।
- व्यापक डेटा निगरानी और सेंसरशिप की नीति।
प्रश्न 75: “Exclusionary Rule” (अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य का निषेध) भारत और अमेरिका में कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत:
- कोई सख्त “Exclusionary Rule” नहीं है।
- न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य स्वीकार कर सकता है।
- अमेरिका:
- “Mapp v. Ohio (1961)” के तहत अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्य अस्वीकार्य।
- “Fruit of the Poisonous Tree Doctrine” लागू।
प्रश्न 76: भारत और जर्मनी में “Insanity Defense” (पागलपन का बचाव) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- IPC धारा 84 के तहत केवल पूर्ण मानसिक अस्थिरता पर बचाव संभव।
- जर्मनी:
- मानसिक विकार होने पर “Diminished Responsibility” (घटित उत्तरदायित्व) का प्रावधान।
प्रश्न 77: “White Collar Crimes” (सफेदपोश अपराध) के लिए भारत और अमेरिका में क्या दंड प्रक्रियाएँ हैं?
उत्तर:
- भारत: प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI और SEBI जांच करते हैं।
- अमेरिका: FBI और SEC द्वारा कठोर नियामक कानून लागू।
प्रश्न 78: भारत और सऊदी अरब में “Capital Punishment” (मृत्युदंड) कैसे दिया जाता है?
उत्तर:
- भारत: दुर्लभतम मामलों में ही दी जाती है, जैसे निर्भया केस।
- सऊदी अरब: सार्वजनिक रूप से सिर कलम करने जैसे कठोर दंड लागू।
प्रश्न 79: भारत, अमेरिका और रूस में “Parole System” (परोल प्रणाली) में क्या अंतर है?
उत्तर:
| देश | परोल नीति |
|——–|————-|
| भारत | राज्य सरकार की अनुशंसा पर दी जाती है। |
| अमेरिका | “Federal Parole System” अधिकांश मामलों में निष्क्रिय। |
| रूस | गंभीर अपराधों में परोल कठिनाई से मिलती है। |
प्रश्न 80: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन न्यायिक सुधारों को समझने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 81: भारत और अमेरिका में “Juvenile Justice System” (किशोर न्याय प्रणाली) में क्या अंतर है?
उत्तर:
| तत्व | भारत | अमेरिका |
|———|———|———–|
| कानून | Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 | Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act, 1974 |
| अपराध की उम्र सीमा | 18 वर्ष से कम | 18 वर्ष से कम, लेकिन कुछ मामलों में नाबालिगों को वयस्कों की तरह ट्रायल किया जा सकता है |
| सजा | सुधारात्मक दृष्टिकोण, मृत्युदंड नहीं | कुछ मामलों में किशोरों को आजीवन कारावास |
प्रश्न 82: भारत और कनाडा में “Extradition Laws” (प्रत्यर्पण कानून) कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत: “Extradition Act, 1962” लागू, प्रत्यर्पण संधि आवश्यक।
- कनाडा: “Extradition Act, 1999” लागू, प्रत्यर्पण के लिए मजबूत मानवाधिकार सुरक्षा।
प्रश्न 83: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Public Prosecutor” (लोक अभियोजक) की क्या भूमिका है?
उत्तर:
- भारत: CrPC की धारा 24 के तहत लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।
- दक्षिण अफ्रीका: राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (NPA) अभियोजकों की नियुक्ति करता है।
प्रश्न 84: भारत और जापान में “Criminal Investigation Process” (आपराधिक जांच प्रक्रिया) में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत: पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच करती है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में।
- जापान: अभियोजक की भूमिका जांच में अधिक महत्वपूर्ण होती है।
प्रश्न 85: भारत और ब्रिटेन में “Right to Silence” (मौन रहने का अधिकार) कैसे लागू होता है?
उत्तर:
- भारत: अनुच्छेद 20(3) के तहत आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- ब्रिटेन: “Criminal Justice and Public Order Act, 1994” के तहत चुप्पी रखने पर नकारात्मक अनुमान लगाया जा सकता है।
प्रश्न 86: “Cyber Crimes” (साइबर अपराध) से निपटने के लिए भारत और अमेरिका में क्या कानून हैं?
उत्तर:
- भारत: “Information Technology Act, 2000” लागू।
- अमेरिका: “Computer Fraud and Abuse Act, 1986” लागू।
प्रश्न 87: भारत और जर्मनी में “Prison System” (कारागार प्रणाली) कैसे भिन्न है?
उत्तर:
- भारत: जेल सुधार धीरे-धीरे हो रहे हैं, भीड़भाड़ एक समस्या है।
- जर्मनी: सुधारात्मक दृष्टिकोण, कैदियों के पुनर्वास पर जोर।
प्रश्न 88: भारत, अमेरिका और फ्रांस में “Pardon and Clemency” (माफी और दया याचिका) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
| देश | माफी का प्रावधान |
|——–|—————-|
| भारत | राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत माफी दे सकते हैं। |
| अमेरिका | राष्ट्रपति पूर्ण माफी दे सकते हैं। |
| फ्रांस | राष्ट्रपति विशेष मामलों में माफी प्रदान कर सकते हैं। |
प्रश्न 89: भारत और सिंगापुर में “Death Sentence Execution” (मृत्युदंड निष्पादन) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत: फांसी द्वारा निष्पादन (फांसीघर में)।
- सिंगापुर: फांसी द्वारा निष्पादन, मादक पदार्थ तस्करी के लिए भी मृत्युदंड।
प्रश्न 90: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया का अध्ययन न्यायिक प्रणालियों की प्रभावशीलता को समझने में सहायक होता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 91: भारत और ब्रिटेन में “Bail” (जमानत) देने की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- जमानत देने की प्रक्रिया न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है।
- मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय दोनों के पास जमानत देने का अधिकार है।
- ब्रिटेन:
- “Bail Act, 1976” के तहत जमानत दी जाती है, हालांकि कुछ मामलों में, जैसे आतंकवादी अपराधों में, जमानत की अनुमति नहीं होती।
प्रश्न 92: भारत और जापान में “Corruption Laws” (भ्रष्टाचार कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Prevention of Corruption Act, 1988” लागू।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सजा का प्रावधान।
- जापान:
- “Unfair Competition Prevention Act” के तहत भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध।
- कानून की प्रवर्तन प्रक्रिया कठोर है।
प्रश्न 93: भारत और जर्मनी में “Police Accountability” (पुलिस की जिम्मेदारी) कैसे नियंत्रित होती है?
उत्तर:
- भारत:
- पुलिस की जिम्मेदारी का पालन “National Human Rights Commission” और “State Human Rights Commission” द्वारा किया जाता है।
- कुछ मामलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है।
- जर्मनी:
- पुलिस के कामकाज की जिम्मेदारी “Federal Court” और अन्य न्यायिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रियाएँ लागू हैं।
प्रश्न 94: भारत और फ्रांस में “Search and Seizure” (तलाशी और जब्ती) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- “Criminal Procedure Code (CrPC)” की धारा 100 के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया निर्धारित होती है।
- तलाशी के दौरान एक गवाह की उपस्थिति आवश्यक होती है।
- फ्रांस:
- “Code of Criminal Procedure” के तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया होती है।
- पुलिस को जाँच करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हालांकि न्यायालय की मंजूरी आवश्यक होती है।
प्रश्न 95: भारत और अमेरिका में “Self-defense” (आत्मरक्षा) का अधिकार कैसे लागू होता है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 96-106 में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है।
- यह अधिकार केवल असामान्य परिस्थितियों में लागू होता है।
- अमेरिका:
- “Stand Your Ground Law” के तहत, कुछ राज्यों में आत्मरक्षा का अधिकार बिना किसी कर्तव्य के उपयोग करने की अनुमति है।
- न्यायालय में यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि आत्मरक्षा वैध थी।
प्रश्न 96: भारत और दक्षिण कोरिया में “Rehabilitation of Offenders” (अपराधियों का पुनर्वास) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- पुनर्वास की प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान अपराधियों के सुधार पर होता है।
- “Prisoners’ Welfare Fund” और “Rehabilitation Programs” लागू हैं।
- दक्षिण कोरिया:
- जेलों में सुधारात्मक उपायों पर जोर दिया जाता है।
- कैदियों के पुनर्वास के लिए “Correctional Facilities” के जरिए मानसिक और शारीरिक सुधार किया जाता है।
प्रश्न 97: भारत और ब्रिटेन में “Sentencing” (सजा देना) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- न्यायालय सजा देने में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का पालन करता है।
- गंभीर अपराधों के लिए सजा का निर्धारण अपराध के प्रकार और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
- ब्रिटेन:
- सजा का निर्धारण “Sentencing Council” के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है।
- न्यायालय पुनः अपराधी की स्थिति और सुधार की संभावना पर विचार करता है।
प्रश्न 98: भारत और पाकिस्तान में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत:
- “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” (UAPA) के तहत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- संदिग्धों की गिरफ्तारी और पूछताछ में विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं।
- पाकिस्तान:
- “Anti-Terrorism Act, 1997” लागू।
- आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है।
प्रश्न 99: भारत और चीन में “Military Courts” (सैन्य न्यायालय) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- “Army Act, 1950” और “Navy Act, 1957” के तहत सैन्य न्यायालयों की स्थापना।
- सैन्य कर्मियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया।
- चीन:
- “Military Court” के तहत सैन्य कर्मियों के खिलाफ सुनवाई होती है।
- सैन्य न्यायालयों की कार्यवाही राज्य की सुरक्षा के लिहाज से नियंत्रित होती है।
प्रश्न 100: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न देशों के न्यायिक प्रणाली, सुधारात्मक प्रक्रियाओं, और कानूनी दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े और भी महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 101: भारत और ब्रिटेन में “Jury System” (जूरी प्रणाली) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- जूरी प्रणाली का अभ्यास 1960 में समाप्त कर दिया गया था।
- अब केवल “Judge-led trials” होते हैं।
- ब्रिटेन:
- जूरी प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से गंभीर अपराधों में किया जाता है।
- 12 सदस्यीय जूरी दोष और निर्दोष का निर्णय करती है।
प्रश्न 102: भारत और कनाडा में “Habeas Corpus” (हैबियस कॉर्पस) का अधिकार कैसे लागू होता है?
उत्तर:
- भारत:
- “Article 32” और “Article 226” के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की जा सकती है।
- यह अधिकार अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- कनाडा:
- “Canadian Charter of Rights and Freedoms” के तहत यह अधिकार मौजूद है।
- नागरिकों को अवैध गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की स्थितियों पर सवाल उठाने का अधिकार प्राप्त है।
प्रश्न 103: भारत और रूस में “Crime Prevention” (अपराध की रोकथाम) के उपायों में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- अपराध की रोकथाम के लिए शिक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, और जागरूकता अभियान जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।
- “Community Policing” का प्रचलन बढ़ रहा है।
- रूस:
- अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सुरक्षा सेवाएँ और “Preemptive Measures” का इस्तेमाल किया जाता है।
- कठोर कानूनी प्रावधान और पुलिस निगरानी बढ़ाई गई है।
प्रश्न 104: भारत और स्वीडन में “Witness Protection Program” (गवाह सुरक्षा कार्यक्रम) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- “Witness Protection Scheme, 2018” लागू है।
- गवाहों की सुरक्षा के लिए पहचान बदलने और अन्य सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
- स्वीडन:
- गवाहों की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू हैं।
- गवाहों को छिपाने, स्थान बदलने और गवाही देने के बाद सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है।
प्रश्न 105: भारत और सिंगापुर में “Drug Laws” (मादक पदार्थों से संबंधित कानून) कैसे भिन्न हैं?
उत्तर:
- भारत:
- “Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985” लागू।
- मादक पदार्थों के अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, लेकिन कुछ मामले में सुधारात्मक उपायों का भी प्रावधान है।
- सिंगापुर:
- “Misuse of Drugs Act, 1973” के तहत मादक पदार्थों के अपराधों के लिए सख्त दंड जैसे मृत्युदंड और जीवनभर कारावास दिया जाता है।
प्रश्न 106: भारत और ऑस्ट्रेलिया में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” (UAPA) के तहत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- आतंकवादियों की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- ऑस्ट्रेलिया:
- “Australian Security Intelligence Organisation Act” और “Australian Anti-Terrorism Laws” के तहत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार मिलते हैं, लेकिन कड़े निगरानी उपाय भी होते हैं।
प्रश्न 107: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में “Police Brutality” (पुलिस क्रूरता) से निपटने के लिए क्या उपाय हैं?
उत्तर:
- भारत:
- “National Human Rights Commission” (NHRC) और “State Human Rights Commissions” द्वारा पुलिस क्रूरता की जांच की जाती है।
- कुछ राज्यों में पुलिस सुधार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार धीमे हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
- “Civil Rights Division” के तहत पुलिस क्रूरता की शिकायतों पर जांच की जाती है।
- हाल के वर्षों में पुलिस सुधार और अधिक पारदर्शिता की मांग बढ़ी है।
प्रश्न 108: भारत और जर्मनी में “Mental Health and Criminal Responsibility” (मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक जिम्मेदारी) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- IPC की धारा 84 के तहत मानसिक विकृति के कारण अपराधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- “Mental Health Act, 1987” और “Mental Healthcare Act, 2017” मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में सुधार की दिशा में कार्यरत हैं।
- जर्मनी:
- मानसिक विकारों के कारण अपराधियों को “Diminished Responsibility” का प्रावधान होता है।
- जर्मन दंड संहिता में मानसिक रोगी की स्थिति का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा किया जाता है।
प्रश्न 109: भारत और अफगानिस्तान में “Judicial Independence” (न्यायिक स्वतंत्रता) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- संविधान के अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124 के तहत न्यायपालिका स्वतंत्र है।
- न्यायिक निर्णयों पर किसी भी बाहरी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है।
- अफगानिस्तान:
- अफगानिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता का पालन संविधान में किया गया है, लेकिन राजनीतिक दबाव और न्यायिक भ्रष्टाचार की समस्याएँ हैं।
प्रश्न 110: निष्कर्ष
तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया अध्ययन विभिन्न देशों के कानूनों और न्यायिक प्रथाओं की समीक्षा करता है, जिससे हम विभिन्न कानूनी संरचनाओं की समानताएँ और भिन्नताएँ समझ सकते हैं। यह न केवल न्यायिक सुधार में मदद करता है, बल्कि वैश्विक कानूनी परिप्रेक्ष्य में भी विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
यहाँ तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 111 से 200 तक दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे।
प्रश्न 111: भारत और चीन में “Right to Fair Trial” (न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक उचित और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार प्राप्त है।
- चीन:
- चीन में न्यायिक प्रक्रिया पर राज्य का नियंत्रण होता है और एक निष्पक्ष परीक्षण की संभावना सीमित होती है, विशेष रूप से राजनीतिक मामलों में।
प्रश्न 112: भारत और कनाडा में “Double Jeopardy” (दोहरी सजा) का सिद्धांत कैसे लागू होता है?
उत्तर:
- भारत:
- “Article 20(2)” के तहत दोहरी सजा का निषेध है, यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती।
- कनाडा:
- “Section 11(h)” के तहत दोहरी सजा का सिद्धांत लागू है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 113: भारत और जर्मनी में “Prosecutor’s Role” (अभियोजक की भूमिका) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- अभियोजक न्यायालय में सरकार की ओर से मुकदमा चलाता है, और उसका उद्देश्य अपराधियों को सजा दिलाना है।
- जर्मनी:
- अभियोजक की भूमिका में एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करना होता है, और वह न्याय का पक्ष लेने की बजाय तथ्यों और कानून का पालन करता है।
प्रश्न 114: भारत और फ्रांस में “Bail Laws” (जमानत कानून) में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- “Criminal Procedure Code” की धारा 437 और 439 के तहत जमानत दी जाती है, जो न्यायालय की विवेकाधीन होती है।
- फ्रांस:
- जमानत का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है, और यदि आरोपी को विशेष परिस्थितियों में जोखिम नहीं माना जाता, तो जमानत दी जाती है।
प्रश्न 115: भारत और अमेरिका में “Capital Punishment” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को केवल गंभीर मामलों में स्वीकार किया है।
- अमेरिका:
- मृत्युदंड कुछ राज्यों में वैध है, जबकि कुछ राज्यों में यह कानून समाप्त हो चुका है।
- यह अपराध के प्रकार और राज्य के कानून पर निर्भर करता है।
प्रश्न 116: भारत और ब्रिटेन में “Witness Testimony” (गवाह की गवाही) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- गवाहों की गवाही को न्यायालय में सीधे तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और जिरह की प्रक्रिया के दौरान गवाह से सवाल किए जाते हैं।
- ब्रिटेन:
- गवाहों की गवाही को “Oral Testimony” और “Written Statements” दोनों के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।
प्रश्न 117: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Racial Discrimination Laws” (नस्लीय भेदभाव कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और 17 के तहत नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रावधान हैं।
- दक्षिण अफ्रीका:
- “Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, 2000” के तहत नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कठोर उपाय हैं।
प्रश्न 118: भारत और जापान में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- मृत्युदंड भारतीय न्याय प्रणाली में केवल गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी, और हत्या।
- जापान:
- जापान में मृत्युदंड के मामले अत्यंत सीमित होते हैं, और यह हत्या, आतंकवाद और युद्ध अपराधों के लिए दिया जाता है।
प्रश्न 119: भारत और पाकिस्तान में “Military Courts” (सैन्य न्यायालय) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- “Army Act, 1950” के तहत सैन्य न्यायालयों का गठन किया गया है।
- केवल सैन्य कर्मियों को सैन्य न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।
- पाकिस्तान:
- पाकिस्तान में सैन्य न्यायालयों का गठन “Anti-Terrorism Act” के तहत किया जाता है।
- आतंकवाद के मामलों में सैन्य न्यायालयों द्वारा सुनवाई की जाती है।
प्रश्न 120: भारत और रूस में “Prison System” (जेल प्रणाली) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय जेलों में सुधारात्मक उपायों की कमी है, और भीड़-भाड़ एक गंभीर समस्या है।
- हालाँकि, सुधारात्मक जेल प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।
- रूस:
- रूस की जेल प्रणाली में अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है, और यह मानवीय अधिकारों की कमी से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
प्रश्न 121: भारत और कनाडा में “Criminal Liability of Corporations” (कंपनियों की आपराधिक जिम्मेदारी) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- कंपनियों को “Indian Penal Code” और “Companies Act, 2013” के तहत आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।
- कंपनियों के निदेशक और अधिकारी अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।
- कनाडा:
- “Canadian Criminal Code” के तहत कंपनियों को आपराधिक दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, विशेषकर आर्थिक अपराधों में।
प्रश्न 122: भारत और दक्षिण कोरिया में “Anti-Corruption Laws” (भ्रष्टाचार विरोधी कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Prevention of Corruption Act, 1988” भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून है।
- सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
- दक्षिण कोरिया:
- “Act on Combating Bribery” और “Anti-Corruption and Civil Rights Commission Act” भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत भ्रष्टाचार से निपटते हैं।
प्रश्न 123: भारत और अमेरिका में “Evidence Rules” (साक्ष्य नियम) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Indian Evidence Act, 1872” के तहत साक्ष्य की प्रक्रिया निर्धारित होती है।
- सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत नियम होते हैं।
- अमेरिका:
- “Federal Rules of Evidence” और “State Rules of Evidence” के तहत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डिजिटल डेटा को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए सख्त मानक हैं।
प्रश्न 124: भारत और जर्मनी में “Trial Procedure” (न्यायिक प्रक्रिया) में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- न्यायिक प्रक्रिया में जज और अभियोजक दोनों का कार्य प्रमुख होता है, और यह प्रक्रिया जूरी के बिना होती है।
- जर्मनी:
- जर्मन न्यायिक प्रणाली में अभियोजक को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की भूमिका निभानी होती है।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 125 से 200 तक विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 125: भारत और पाकिस्तान में “Terrorism Laws” (आतंकवाद विरोधी कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967” के तहत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- भारतीय आतंकवाद विरोधी कानूनों में गिरफ्तारियों, संपत्ति की जब्ती, और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- पाकिस्तान:
- “Anti-Terrorism Act, 1997” के तहत आतंकवाद विरोधी कड़े कानून लागू हैं।
- विशेष न्यायालयों द्वारा आतंकवाद के मामलों की सुनवाई की जाती है।
प्रश्न 126: भारत और इंग्लैंड में “Bail System” (जमानत प्रणाली) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- जमानत की प्रक्रिया “Criminal Procedure Code” की धारा 437 और 439 के तहत की जाती है।
- अदालत जमानत देने के दौरान आरोपी के अपराध की गंभीरता और समाज में उसके प्रभाव को ध्यान में रखती है।
- इंग्लैंड:
- जमानत का अधिकार सभी अभियुक्तों को है, लेकिन कुछ मामलों में, विशेषकर गंभीर अपराधों में, अदालत जमानत मना भी कर सकती है।
प्रश्न 127: भारत और ऑस्ट्रेलिया में “Corruption Laws” (भ्रष्टाचार कानून) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- “Prevention of Corruption Act, 1988” भ्रष्टाचार के मामलों को नियंत्रित करता है।
- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- ऑस्ट्रेलिया:
- “Australian Federal Police” और विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही की जाती है।
- “Corruption and Crime Commission” (CCC) भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही का प्रमुख अंग है।
प्रश्न 128: भारत और इजरायल में “National Security Laws” (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” और “National Security Act, 1980” के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानून लागू होते हैं।
- आतंकवादी और अन्य सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं।
- इजरायल:
- “Anti-Terrorism Law” और “Prevention of Infiltration Law” के तहत इजरायल में सुरक्षा के कड़े कानून लागू हैं।
- देश में सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सख्त सुरक्षा प्राधिकरण हैं।
प्रश्न 129: भारत और न्यूजीलैंड में “Defence Rights” (सुरक्षा अधिकार) की क्या स्थिति है?
उत्तर:
- भारत:
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त को अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
- “Criminal Procedure Code” के तहत अभियुक्त को बचाव करने का अवसर दिया जाता है।
- न्यूजीलैंड:
- “Bill of Rights Act, 1990” के तहत अभियुक्त को निष्पक्ष परीक्षण और कानूनी सहायता का अधिकार है।
- अदालत अभियुक्त को बचाव के लिए पर्याप्त समय और अवसर देती है।
प्रश्न 130: भारत और जापान में “Rights of the Accused” (अभियुक्त के अधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- अभियुक्त को अपने बचाव के लिए कानूनी सहायता, उचित परीक्षण और गवाही का अधिकार है।
- संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अभियुक्त को कई अधिकार प्राप्त हैं।
- जापान:
- जापान में अभियुक्त को अपने अधिकारों का पालन करने का अवसर मिलता है, और उसे वकील रखने का अधिकार होता है।
- जापान में गवाही का अधिकार और त्वरित परीक्षण का प्रावधान है।
प्रश्न 131: भारत और स्पेन में “Police Custody” (पुलिस हिरासत) के अधिकार की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- पुलिस हिरासत की अवधि “Criminal Procedure Code” की धारा 57 और 167 के तहत निर्धारित होती है।
- अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखने से पहले न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है।
- स्पेन:
- स्पेन में पुलिस हिरासत को 72 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस अवधि में अभियुक्त को अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए।
प्रश्न 132: भारत और स्वीडन में “Right to Counsel” (कानूनी सहायता का अधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- अभियुक्त को कानूनी सहायता का अधिकार “Criminal Procedure Code” की धारा 303 और 304 के तहत दिया जाता है।
- यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षित है।
- स्वीडन:
- स्वीडन में भी अभियुक्त को कानूनी सहायता का अधिकार है, और यदि वह सक्षम नहीं है तो राज्य द्वारा वकील प्रदान किया जाता है।
प्रश्न 133: भारत और अमेरिका में “Evidence Collection” (साक्ष्य संग्रहण) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Indian Evidence Act, 1872” के तहत साक्ष्य संग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित होती है।
- डिजिटल और भौतिक साक्ष्य दोनों प्रकार के साक्ष्य का न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अमेरिका:
- “Federal Rules of Evidence” के तहत साक्ष्य संग्रहण के मानक निर्धारित किए गए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसकी प्रमाणिकता की जांच की जाती है।
प्रश्न 134: भारत और ब्रिटेन में “Trial in Absentia” (गैरमौजूदगी में मुकदमा) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय कानून में, यदि अभियुक्त मुकदमे के दौरान उपस्थित नहीं होता है, तो अदालत गैरमौजूदगी में मुकदमा चला सकती है।
- हालांकि, गंभीर मामलों में, अभियुक्त की अनुपस्थिति पर विचार किया जाता है।
- ब्रिटेन:
- ब्रिटेन में “Trial in Absentia” का अभ्यास आमतौर पर नहीं किया जाता, लेकिन कुछ स्थितियों में यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति सही ठहराई जाती है, तो मुकदमा चलाया जा सकता है।
प्रश्न 135: भारत और इटली में “Child Criminal Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपचार देने की दिशा में काम किया जाता है।
- इटली:
- इटली में बाल अपराधियों के लिए अलग-अलग न्यायिक प्रक्रिया है।
- “Juvenile Justice System” के तहत बच्चों के अपराध से संबंधित मामलों को विशेष अदालत में सुना जाता है।
प्रश्न 136: भारत और न्यूजीलैंड में “Extradition Laws” (प्रत्यक्षीकरण कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत ने कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ की हैं, और “Extradition Act, 1962” के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया निर्धारित है।
- न्यूजीलैंड:
- “Extradition Act, 1999” के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया संचालित होती है।
- इसमें अपराध की गंभीरता और प्रत्यर्पण की स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है।
प्रश्न 137: भारत और फ्रांस में “Prosecutor’s Independence” (अभियोजक की स्वतंत्रता) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- अभियोजक की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है, लेकिन वह सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।
- अभियोजक अदालत में निष्पक्षता से मामलों की सुनवाई करते हैं।
- फ्रांस:
- फ्रांस में अभियोजक का कार्य स्वतंत्र होता है, और वह न्यायपालिका से अलग होकर अपने कार्य करता है।
प्रश्न 138: भारत और नीदरलैंड्स में “Criminal Jurisdiction” (आपराधिक क्षेत्राधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Criminal Procedure Code” के तहत अपराधों की सुनवाई संबंधित क्षेत्रीय न्यायालय में होती है।
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष अपीलों का अधिकार होता है।
- नीदरलैंड्स:
- नीदरलैंड्स में क्षेत्रीय न्यायालयों के पास अपराधों का क्षेत्राधिकार होता है, और अपील की प्रक्रिया उच्च न्यायालयों के पास होती है।
प्रश्न 139: भारत और कनाडा में “Sentencing” (सजा) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- सजा का निर्धारण अपराध की गंभीरता, आरोपी की पृष्ठभूमि, और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है।
- “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत सजा का निर्धारण किया जाता है।
- कनाडा:
- कनाडा में “Criminal Code” के तहत सजा का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- सजा के दौरान आरोपी की स्थिति, अपराध की प्रकृति और दोषी की सुधारात्मक संभावना को ध्यान में रखा जाता है।
प्रश्न 140: भारत और इंग्लैंड में “Legal Aid” (कानूनी सहायता) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Legal Services Authorities Act, 1987” के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- यह सरकारी प्रणाली के तहत उपलब्ध कराई जाती है।
- इंग्लैंड:
- इंग्लैंड में “Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act, 2012” के तहत कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- यह विधायी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि गरीबों को उचित कानूनी सहायता मिले।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 141 से 200 तक दिए गए हैं:
प्रश्न 141: भारत और अर्जेंटीना में “Police Interrogation” (पुलिस पूछताछ) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को “Criminal Procedure Code” की धारा 50 और 161 के तहत अधिकार होते हैं।
- आरोपी को अपनी गवाही देने से इनकार करने का अधिकार है।
- अर्जेंटीना:
- अर्जेंटीना में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पूछताछ जबरदस्ती न हो।
प्रश्न 142: भारत और अमेरिका में “Self-Incrimination” (आत्म-आपराधीकरण) के अधिकार की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आरोपी को आत्म-आपराधीकरण से बचने का अधिकार है।
- इसका मतलब है कि आरोपी को अपनी गवाही से खुद के खिलाफ कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होती।
- अमेरिका:
- अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत आरोपी को आत्म-आपराधीकरण से बचने का अधिकार है।
- यह अधिकार अदालतों में एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रश्न 143: भारत और इंग्लैंड में “Juvenile Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत बाल अपराधियों को सुधारात्मक तरीके से सजा दी जाती है।
- बाल अपराधियों के लिए विशेष अदालतें हैं।
- इंग्लैंड:
- इंग्लैंड में “Children and Young Persons Act, 1933” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- अदालतें बच्चों की स्थिति और अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्णय देती हैं।
प्रश्न 144: भारत और दक्षिण कोरिया में “Bail and Remand” (जमानत और रिमांड) की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
उत्तर:
- भारत:
- जमानत का अधिकार “Criminal Procedure Code” की धारा 437 और 439 के तहत है।
- रिमांड का आदेश न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए दिया जाता है।
- दक्षिण कोरिया:
- दक्षिण कोरिया में जमानत को लेकर सख्त नियम हैं, और न्यायालय की अनुमति के बिना जमानत नहीं दी जाती।
- रिमांड की अवधि सीमित होती है और इसे न्यायालय द्वारा ही बढ़ाया जाता है।
प्रश्न 145: भारत और जापान में “Compensation to Victims” (पीड़ितों को मुआवजा) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Victim Compensation Scheme” के तहत अपराध के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- न्यायालय पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए आदेश दे सकते हैं।
- जापान:
- जापान में “Crime Victim Compensation Act” के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है।
- पीड़ितों को पुलिस और न्यायालयों के माध्यम से सहायता प्राप्त होती है।
प्रश्न 146: भारत और कनाडा में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड को “Indian Penal Code” के तहत गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे हत्या, आतंकवाद आदि।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असाधारण मामलों में लागू करने का सुझाव दिया है।
- कनाडा:
- कनाडा ने 1976 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था।
- अब यहां केवल आजीवन कारावास या अन्य दंडों का प्रावधान है।
प्रश्न 147: भारत और रूस में “Extradition” (प्रत्यक्षीकरण) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत ने विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ की हैं, और “Extradition Act, 1962” के तहत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- प्रत्यर्पण के मामलों में अपराध की गंभीरता और दोनों देशों के कानूनों का पालन जरूरी है।
- रूस:
- रूस में “Extradition Law” के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया संचालित होती है।
- रूस और अन्य देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौते हैं, और कड़े नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 148: भारत और स्वीडन में “Prison Reforms” (जेल सुधार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जेल सुधारों के तहत अपराधियों को सुधारात्मक उपाय और पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- “Prison Act” के तहत जेलों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
- स्वीडन:
- स्वीडन में जेल सुधार की प्रक्रिया अत्यधिक उन्नत है।
- अपराधियों को जेल में सुधारात्मक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया का पालन कराया जाता है।
प्रश्न 149: भारत और जर्मनी में “Crime Prevention” (अपराध की रोकथाम) की क्या रणनीतियाँ हैं?
उत्तर:
- भारत:
- अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे “Community Policing” और “Surveillance Programs”।
- अपराधियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाता है।
- जर्मनी:
- जर्मनी में अपराध की रोकथाम के लिए “Preventive Police Measures” और “Restorative Justice” कार्यक्रम होते हैं।
- समाज में अपराधीकरण के कारणों को कम करने के लिए व्यापक योजनाएँ लागू की जाती हैं।
प्रश्न 150: भारत और फ्रांस में “Cybercrime Laws” (साइबर अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Information Technology Act, 2000” के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम और निपटान के लिए कानून बनाए गए हैं।
- इसमें हैकिंग, धोखाधड़ी, और ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं।
- फ्रांस:
- फ्रांस में “Cybercrime Law” के तहत साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- फ्रांसीसी पुलिस साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष इकाई स्थापित करती है।
प्रश्न 151: भारत और यूनाइटेड किंगडम में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की व्यवस्था कैसे की जाती है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Witness Protection Scheme” के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- गवाहों के लिए गुमनामी और सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है।
- यूनाइटेड किंगडम:
- ब्रिटेन में “Witness Protection Program” के तहत गवाहों को सुरक्षा और गुमनामी दी जाती है।
- विशेष सुरक्षा प्रबंधों और परिवर्तित पहचान की प्रक्रिया लागू की जाती है।
प्रश्न 152: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Criminal Appeals” (आपराधिक अपील) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- “Criminal Procedure Code” के तहत अभियुक्त को दोषसिद्धि या सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
- अपील उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
- दक्षिण अफ्रीका:
- दक्षिण अफ्रीका में भी अपील की प्रक्रिया संविधान और “Criminal Procedure Act” के तहत संचालित होती है।
- अपील उच्च न्यायालय से की जाती है, और कुछ मामलों में संविधानिक अपील का भी प्रावधान है।
प्रश्न 153: भारत और अमेरिका में “Civil Liberties and Criminal Procedure” (नागरिक स्वतंत्रताएँ और आपराधिक प्रक्रिया) के बीच संतुलन कैसे किया जाता है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में संविधान के तहत नागरिक स्वतंत्रताओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, और आपराधिक प्रक्रिया के दौरान इन स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- न्यायपालिका नागरिक अधिकारों और सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान लागू करती है।
- अमेरिका:
- अमेरिका में संविधान के तहत नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है।
- “Fourth, Fifth, Sixth Amendments” के तहत नागरिकों को आपराधिक प्रक्रिया में सुरक्षा प्रदान की जाती है।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 154 से 200 तक विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 154: भारत और क्यूबा में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” और “National Investigation Agency Act, 2008” के तहत कानून लागू होते हैं।
- इन कानूनों के तहत आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- क्यूबा:
- क्यूबा में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून हैं, जो “Penal Code” और विशेष आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई करते हैं।
- क्यूबा में आतंकवाद से संबंधित अपराधों को गंभीर माना जाता है और उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
प्रश्न 155: भारत और अर्जेंटीना में “Criminal Liability of Corporations” (कॉर्पोरेशनों की आपराधिक जिम्मेदारी) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारतीय कानून के तहत, कंपनियां अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- “Indian Penal Code” और “Companies Act, 2013” के तहत कंपनियों को आपराधिक मामलों में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- अर्जेंटीना:
- अर्जेंटीना में “Corporate Criminal Liability” के तहत कंपनियों और उनके निदेशकों को आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- अर्जेंटीना ने “Corporate Criminal Responsibility” के प्रावधानों को लागू किया है।
प्रश्न 156: भारत और जर्मनी में “Criminal Procedure for Juveniles” (बाल अपराधियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधियों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपाय और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं।
- जर्मनी:
- जर्मनी में भी बाल अपराधियों के लिए अलग से न्यायिक प्रक्रिया है, जो “Youth Criminal Law” के तहत संचालित होती है।
- यहां भी बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया जाता है।
प्रश्न 157: भारत और जापान में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड को “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, जैसे हत्या, आतंकवाद, और दंगे।
- हालांकि, यह बेहद कम मामलों में लागू होता है।
- जापान:
- जापान में मृत्युदंड को गंभीर अपराधों के लिए दिया जाता है, और यह एक लंबे और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है।
- जापान में मृत्युदंड का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है।
प्रश्न 158: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Prosecutorial Discretion” (अभियोजन की विवेकाधीनता) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में अभियोजक को विवेकाधीनता होती है, लेकिन उसे न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अभियोजन का निर्णय सरकार और अभियोजक के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यह उचित और निष्पक्ष होना चाहिए।
- दक्षिण अफ्रीका:
- दक्षिण अफ्रीका में अभियोजन विवेकाधीन होता है, और इसमें न्यायालय की भी भूमिका होती है।
- अभियोजन के निर्णय में सरकारी नीति और न्यायिक विवेक का महत्व होता है।
प्रश्न 159: भारत और ऑस्ट्रेलिया में “Bail Process” (जमानत प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जमानत देने की प्रक्रिया “Criminal Procedure Code” की धारा 437 और 439 के तहत होती है।
- अदालत जमानत देने के दौरान अभियुक्त की जमानत, अपराध की गंभीरता, और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखती है।
- ऑस्ट्रेलिया:
- ऑस्ट्रेलिया में जमानत की प्रक्रिया “Bail Act, 1977” के तहत होती है।
- इसमें अभियुक्त की जमानत की स्थिति और अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत दी जाती है।
प्रश्न 160: भारत और स्वीडन में “Cyber Crime Laws” (साइबर अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Information Technology Act, 2000” के तहत साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जाता है।
- इसमें हैकिंग, धोखाधड़ी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, और अन्य साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- स्वीडन:
- स्वीडन में भी साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े कानून हैं।
- “Swedish Penal Code” और अन्य कानूनों के तहत साइबर अपराधों को गंभीर माना जाता है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 161: भारत और यूनाइटेड किंगडम में “Police Use of Force” (पुलिस द्वारा बल का उपयोग) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस को बल का उपयोग “Criminal Procedure Code” और “Indian Penal Code” के तहत सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- पुलिस को अत्यधिक बल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, और यह केवल आत्मरक्षा या अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किया जा सकता है।
- यूनाइटेड किंगडम:
- ब्रिटेन में पुलिस को बल का प्रयोग केवल अपनी सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
- “Police and Criminal Evidence Act, 1984” के तहत पुलिस को बल का उपयोग नियंत्रित और आवश्यक परिस्थितियों में किया जाता है।
प्रश्न 162: भारत और फ्रांस में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की व्यवस्था कैसे की जाती है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में गवाहों की सुरक्षा के लिए “Witness Protection Scheme, 2018” के तहत प्रावधान किए गए हैं।
- गवाहों को संरक्षण, गुमनामी, और विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं।
- फ्रांस:
- फ्रांस में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए “Witness Protection Program” लागू है।
- गवाहों की गुमनामी और सुरक्षा के लिए विशेष प्राधिकरण होते हैं।
प्रश्न 163: भारत और कनाडा में “Bail for Serious Offenses” (गंभीर अपराधों के लिए जमानत) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में गंभीर अपराधों के लिए जमानत का प्रावधान “Criminal Procedure Code” के तहत है।
- गंभीर अपराधों जैसे हत्या, दंगे, और आतंकवाद के मामलों में जमानत देने में अदालत सतर्क रहती है।
- कनाडा:
- कनाडा में भी गंभीर अपराधों के मामलों में जमानत का प्रावधान है, लेकिन अदालत यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त जमानत मिलने के बाद समाज के लिए खतरे का कारण न बने।
प्रश्न 164: भारत और मैक्सिको में “Corruption Laws” (भ्रष्टाचार कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Prevention of Corruption Act, 1988” और “Central Vigilance Commission Act” के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून हैं।
- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- मैक्सिको:
- मैक्सिको में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हैं।
- “Federal Anti-Corruption Law” और “National Anticorruption System” के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 165: भारत और इटली में “Criminal Jurisdiction” (आपराधिक क्षेत्राधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के तहत की जाती है।
- न्यायालयों को विशेष मामलों में अपील और सुधारात्मक निर्णय लेने का अधिकार होता है।
- इटली:
- इटली में आपराधिक मामलों की सुनवाई “Criminal Procedure Code” के तहत की जाती है।
- क्षेत्रीय न्यायालयों के पास मामूली मामलों की सुनवाई होती है, जबकि गंभीर मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है।
प्रश्न 166: भारत और दक्षिण कोरिया में “Criminal Procedure” (आपराधिक प्रक्रिया) की तुलना करें।
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Criminal Procedure Code” (CrPC) के तहत अपराधों की प्रक्रिया संचालित होती है।
- इसमें गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, परीक्षण, और सजा की प्रक्रिया शामिल है।
- दक्षिण कोरिया:
- दक्षिण कोरिया में भी एक स्पष्ट “Criminal Procedure Act
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 167 से 200 तक विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 167: भारत और न्यूजीलैंड में “Criminal Procedure for Juveniles” (बाल अपराधियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधियों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- न्यूजीलैंड:
- न्यूजीलैंड में बाल अपराधियों के लिए “Children, Young Persons, and Their Families Act” के तहत न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- यहां बाल अपराधियों को सुधारात्मक कार्यों और सामाजिक पुनर्वास के लिए सुविधाएं दी जाती हैं।
प्रश्न 168: भारत और सिंगापुर में “Cybercrime Laws” (साइबर अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में साइबर अपराधों को “Information Technology Act, 2000” के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- इसमें हैकिंग, धोखाधड़ी, और अन्य साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- सिंगापुर:
- सिंगापुर में “Computer Misuse and Cybersecurity Act” के तहत साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जाता है।
- यहां भी साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त सजा और दंड की व्यवस्था है।
प्रश्न 169: भारत और कनाडा में “Sentencing Process” (सजा प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में सजा की प्रक्रिया “Criminal Procedure Code” (CrPC) के तहत होती है।
- अपराध की गंभीरता, आरोपी की पृष्ठभूमि, और मामले के तथ्यों के आधार पर सजा दी जाती है।
- कनाडा:
- कनाडा में सजा की प्रक्रिया “Criminal Code of Canada” के तहत होती है।
- सजा के निर्धारण में न्यायालय आरोपी की स्थिति, पुनर्वास क्षमता, और समाज पर अपराध के प्रभाव को ध्यान में रखता है।
प्रश्न 170: भारत और ब्राजील में “Extradition” (प्रत्यक्षीकरण) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Extradition Act, 1962” के तहत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया संचालित होती है।
- यह दोनों देशों के बीच समझौते और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर होता है।
- ब्राजील:
- ब्राजील में भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया “International Extradition Treaty” और “Penal Code” के तहत होती है।
- ब्राजील विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि करता है और न्यायालय के माध्यम से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लागू होती है।
प्रश्न 171: भारत और पाकिस्तान में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद के खिलाफ “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” के तहत कार्रवाई की जाती है।
- इसमें आतंकवादी संगठनों और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।
- पाकिस्तान:
- पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ “Anti-Terrorism Act, 1997” के तहत कड़े कानून हैं।
- आतंकवाद से संबंधित अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है, और इन पर कठोर दंड लागू किया जाता है।
प्रश्न 172: भारत और जर्मनी में “Police Use of Force” (पुलिस द्वारा बल का प्रयोग) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस द्वारा बल का प्रयोग “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत नियंत्रित होता है।
- पुलिस को बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा या गिरफ्तार करने के लिए किया जा सकता है।
- जर्मनी:
- जर्मनी में पुलिस को बल का प्रयोग “Police Law” के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- जर्मनी में पुलिस को बल का प्रयोग तब किया जा सकता है जब अन्य उपाय असफल हो जाते हैं और स्थिति अत्यधिक गंभीर हो।
प्रश्न 173: भारत और कनाडा में “Prison Reforms” (जेल सुधार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जेल सुधारों के तहत “Prison Act” और विभिन्न सुधारात्मक योजनाओं के तहत प्रयास किए जा रहे हैं।
- इसके अंतर्गत अपराधियों के पुनर्वास, सुधारात्मक प्रशिक्षण, और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है।
- कनाडा:
- कनाडा में जेल सुधार की प्रक्रिया में “Correctional Service Canada” की प्रमुख भूमिका है।
- कनाडा में अपराधियों के पुनर्वास और समाज में पुनः प्रवेश के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
प्रश्न 174: भारत और इटली में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Witness Protection Scheme, 2018” के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- गवाहों की गुमनामी, जीवन सुरक्षा, और उनके परिवार के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं।
- इटली:
- इटली में भी गवाह सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम हैं।
- गवाहों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है और उनकी पहचान बदलने की प्रक्रिया भी उपलब्ध होती है।
प्रश्न 175: भारत और अमेरिका में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड को विशेष मामलों में लागू किया जाता है, जैसे गंभीर हत्या, आतंकवाद, और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इसे असाधारण मामलों तक सीमित करने का सुझाव देता है।
- अमेरिका:
- अमेरिका में मृत्युदंड लागू करने की प्रक्रिया राज्य और संघीय स्तर पर भिन्न होती है।
- कई राज्य मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ राज्य इसे गंभीर अपराधों के लिए बनाए रखते हैं।
प्रश्न 176: भारत और स्वीडन में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” और “National Investigation Agency Act, 2008” के तहत कानून लागू होते हैं।
- इन कानूनों के तहत आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।
- स्वीडन:
- स्वीडन में आतंकवाद के खिलाफ कानून “Terrorism Act” के तहत कार्यान्वित होते हैं।
- स्वीडन में आतंकवाद को एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसे रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाते हैं।
प्रश्न 177: भारत और फ्रांस में “Cybercrime Laws” (साइबर अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में साइबर अपराधों के लिए “Information Technology Act, 2000” लागू है।
- इसमें हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, और अन्य साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
- फ्रांस:
- फ्रांस में “Cybercrime Law” के तहत साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जाता है।
- फ्रांसीसी पुलिस और न्यायपालिका साइबर अपराधों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करती है।
प्रश्न 178: भारत और यूनाइटेड किंगडम में “Extradition Process” (प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया “Extradition Act, 1962” के तहत होती है।
- यह प्रक्रिया दो देशों के बीच न्यायिक समझौतों और द्विपक्षीय संधियों पर आधारित होती है।
- यूनाइटेड किंगडम:
- ब्रिटेन में भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया कानून और द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित है।
- ब्रिटेन और अन्य देशों के बीच प्रत्यर्पण की प्रक्रिया संधियों के तहत चलती है।
प्रश्न 179: भारत और इटली में “Police Interrogation” (पुलिस पूछताछ) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- आरोपी को “Criminal Procedure Code” की धारा 50 के तहत गिरफ्तारी और पूछताछ के अधिकार होते हैं।
- इटली:
- इटली में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति होती है।
- पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने अधिकारों की जानकारी दी जाती है।
प्रश्न 180: भारत और जापान में “Juvenile Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधियों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” लागू है।
- बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपाय और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं।
- जापान:
- जापान में “Juvenile Law” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- यहां भी बच्चों को सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत न्याय दिया जाता है।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 181 से 200 तक विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 181: भारत और रूस में “Criminal Liability of Corporations” (कॉर्पोरेशनों की आपराधिक जिम्मेदारी) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Companies Act, 2013” और “Indian Penal Code” के तहत कंपनियां अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं।
- एक कंपनी को आपराधिक अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, विशेषकर जब उसके निदेशक या अधिकारी अपराध करते हैं।
- रूस:
- रूस में भी कंपनियों की आपराधिक जिम्मेदारी है, और “Criminal Code of the Russian Federation” के तहत कंपनियों और उनके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- रूस में कॉर्पोरेशनों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, और अन्य अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
प्रश्न 182: भारत और स्पेन में “Habeas Corpus” (हैबियस कॉर्पस) का महत्व क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Habeas Corpus” का अधिकार संविधान के तहत सुनिश्चित किया गया है, जो किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने का अधिकार है।
- यह एक मौलिक अधिकार है, और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के खिलाफ किया जा सकता है।
- स्पेन:
- स्पेन में भी “Habeas Corpus” का अधिकार संविधान में निहित है।
- किसी भी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए इसे अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रश्न 183: भारत और जर्मनी में “Criminal Procedure for Juveniles” (बाल अपराधियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधियों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं।
- जर्मनी:
- जर्मनी में “Youth Criminal Law” के तहत बच्चों और किशोरों के लिए अलग से न्यायिक प्रक्रिया है।
- जर्मनी में बाल अपराधियों को पुनर्वास और सुधारात्मक उपायों के तहत न्याय दिया जाता है।
प्रश्न 184: भारत और दक्षिण कोरिया में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Witness Protection Scheme, 2018” के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इसमें गवाहों की गुमनामी, सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण और उनकी पहचान को बदलने के प्रावधान हैं।
- दक्षिण कोरिया:
- दक्षिण कोरिया में गवाह सुरक्षा के लिए “Witness Protection Act” है।
- इसमें गवाहों को सुरक्षा, गुमनाम पहचान, और स्थानांतरण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रश्न 185: भारत और यूएसए में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड का प्रावधान विशेष अपराधों के लिए होता है, जैसे हत्या, आतंकवाद, और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध।
- यह केवल असाधारण मामलों में दिया जाता है।
- यूएसए:
- अमेरिका में मृत्युदंड की स्थिति राज्य स्तर पर भिन्न होती है।
- कुछ राज्य मृत्युदंड का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य इसे समाप्त कर चुके हैं।
प्रश्न 186: भारत और ब्रिटेन में “Police Use of Force” (पुलिस द्वारा बल का प्रयोग) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस द्वारा बल का प्रयोग “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत सीमित परिस्थितियों में किया जाता है।
- पुलिस को बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा या गिरफ्तारी के लिए किया जा सकता है।
- ब्रिटेन:
- ब्रिटेन में पुलिस को बल का प्रयोग “Police and Criminal Evidence Act, 1984” और “Human Rights Act, 1998” के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- पुलिस को बल का प्रयोग आवश्यकता और अनुपातिकता के आधार पर किया जाता है।
प्रश्न 187: भारत और कनाडा में “Prosecutorial Discretion” (अभियोजन की विवेकाधीनता) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में अभियोजक को विवेकाधीनता होती है, लेकिन वह न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित होता है।
- अभियोजन का निर्णय सरकार और अभियोजक के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यह उचित और निष्पक्ष होना चाहिए।
- कनाडा:
- कनाडा में अभियोजक को विवेकाधीनता होती है, और न्यायपालिका की भूमिका होती है।
- अभियोजक को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किस मामले में अभियोग चलाना है और किसे नहीं।
प्रश्न 188: भारत और फ्रांस में “Prison Reforms” (जेल सुधार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जेल सुधारों के लिए “Prison Act” और अन्य सुधारात्मक योजनाओं के तहत काम किया जाता है।
- सुधारात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास और समाज में उनका पुनः प्रवेश करना है।
- फ्रांस:
- फ्रांस में “Prison Reform Act” के तहत जेल सुधारों के प्रयास किए जाते हैं।
- यहां भी अपराधियों के पुनर्वास और सुधारात्मक उपायों पर जोर दिया जाता है।
प्रश्न 189: भारत और ऑस्ट्रेलिया में “Bail for Serious Offenses” (गंभीर अपराधों के लिए जमानत) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में गंभीर अपराधों के लिए जमानत देने का प्रावधान “Criminal Procedure Code” के तहत है।
- गंभीर अपराधों जैसे हत्या, आतंकवाद, और दंगे के मामलों में जमानत देने के लिए अदालत कड़ी जांच करती है।
- ऑस्ट्रेलिया:
- ऑस्ट्रेलिया में गंभीर अपराधों के लिए जमानत देने की प्रक्रिया “Bail Act” के तहत होती है।
- जमानत का निर्णय अदालत के विवेक और अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।
प्रश्न 190: भारत और जापान में “Juvenile Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत बाल अपराधियों के लिए अलग से न्यायिक प्रक्रिया है।
- बाल अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपाय और पुनर्वास की व्यवस्था है।
- जापान:
- जापान में “Juvenile Law” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- यहां बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास की प्रक्रिया के तहत न्याय मिलता है।
प्रश्न 191: भारत और पाकिस्तान में “Corruption Laws” (भ्रष्टाचार कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Prevention of Corruption Act, 1988” और अन्य कानूनों के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है।
- पाकिस्तान:
- पाकिस्तान में “National Accountability Bureau Ordinance, 1999” के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
- यहां भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं।
प्रश्न 192: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड का प्रावधान गंभीर अपराधों के लिए होता है, जैसे हत्या, आतंकवाद, और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराध।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इसे असाधारण मामलों तक सीमित करने का सुझाव देता है।
- दक्षिण अफ्रीका:
- दक्षिण अफ्रीका में मृत्युदंड को 1995 में समाप्त कर दिया गया था।
- वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न 193: भारत और यूके में “Extradition Process” (प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया “Extradition Act, 1962” के तहत होती है।
- भारत अन्य देशों से अपराधियों को प्रत्यर्पित करने के लिए संधियों का पालन करता है।
- यूके:
- ब्रिटेन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया कानून और संधियों पर आधारित है।
- ब्रिटेन विभिन्न देशों से अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए समझौते करता है।
प्रश्न 194: भारत और सिंगापुर में “Cybercrime Laws” (साइबर अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में साइबर अपराधों के लिए “Information Technology Act, 2000” लागू है।
- इस कानून के तहत साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, धोखाधड़ी, और ऑनलाइन अपराधों से निपटा जाता है।
- सिंगापुर:
- सिंगापुर में “Computer Misuse and Cybersecurity Act” के तहत साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जाता
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से जुड़े प्रश्न 195 से 200 तक विस्तार से दिए गए हैं:
प्रश्न 195: भारत और दक्षिण कोरिया में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद के खिलाफ “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” के तहत कठोर प्रावधान हैं।
- इसमें आतंकवादी संगठनों, आतंकी फंडिंग, और आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
- दक्षिण कोरिया:
- दक्षिण कोरिया में आतंकवाद के खिलाफ “Anti-Terrorism Act” के तहत कड़े कानून हैं।
- यहां आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर उपायों का पालन किया जाता है।
प्रश्न 196: भारत और फ्रांस में “Sexual Offences Laws” (यौन अपराध कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में यौन अपराधों के लिए “Indian Penal Code” और “Criminal Law (Amendment) Act, 2013” के तहत सख्त कानून हैं।
- इसमें बलात्कार, छेड़छाड़, और अन्य यौन अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा और दंड का प्रावधान है।
- फ्रांस:
- फ्रांस में यौन अपराधों के खिलाफ “French Penal Code” के तहत सख्त कानून हैं।
- फ्रांस में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में कठोर सजा दी जाती है और गवाहों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है।
प्रश्न 197: भारत और कनाडा में “Double Jeopardy” (द्विगुणित दंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Double Jeopardy” का सिद्धांत “Constitution of India” के अनुच्छेद 20(2) के तहत दिया गया है।
- इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती।
- कनाडा:
- कनाडा में भी “Double Jeopardy” का सिद्धांत “Canadian Charter of Rights and Freedoms” के तहत लागू है।
- इसके अनुसार, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियुक्त नहीं ठहराया जा सकता।
प्रश्न 198: भारत और जापान में “Death Penalty” (मृत्युदंड) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में मृत्युदंड का प्रावधान “Indian Penal Code” और अन्य विशेष कानूनों के तहत है।
- इसे गंभीर अपराधों के लिए लागू किया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असाधारण मामलों तक सीमित करने का सुझाव दिया है।
- जापान:
- जापान में मृत्युदंड का प्रावधान है, और यह गंभीर अपराधों के लिए लागू होता है।
- हालांकि, जापान में मृत्युदंड का उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है, और यह एक संविदानिक विवाद का विषय है।
प्रश्न 199: भारत और दक्षिण अफ्रीका में “Prison Reforms” (जेल सुधार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जेल सुधारों के लिए “Prison Act” और विभिन्न सुधारात्मक योजनाओं के तहत प्रयास किए जाते हैं।
- यहां अपराधियों के पुनर्वास और सुधारात्मक उपायों पर ध्यान दिया जाता है।
- दक्षिण अफ्रीका:
- दक्षिण अफ्रीका में “Correctional Services Act” के तहत जेल सुधारों की प्रक्रिया लागू है।
- यहां भी अपराधियों के पुनर्वास, शिक्षा, और सुधारात्मक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाती है।
प्रश्न 200: भारत और स्वीडन में “Police Use of Force” (पुलिस द्वारा बल का प्रयोग) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस द्वारा बल का प्रयोग “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत नियंत्रित होता है।
- बल का प्रयोग तब किया जा सकता है जब किसी अपराधी को गिरफ्तार करना हो या आत्मरक्षा के लिए हो।
- स्वीडन:
- स्वीडन में पुलिस द्वारा बल का प्रयोग “Swedish Police Act” के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- स्वीडन में पुलिस को बल का प्रयोग बहुत सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है, और इसके लिए अनुपातिकता और आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं:
प्रश्न 201: भारत और नॉर्वे में “Bail Process” (जमानत प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में जमानत का प्रावधान “Criminal Procedure Code” (CrPC) के तहत है।
- जमानत केवल किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद दी जाती है, जब आरोपी को न्यायालय द्वारा राहत मिलती है।
- जमानत की प्रक्रिया अपराध की गंभीरता, आरोपी की पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि और संभावित साक्ष्यों के आधार पर होती है।
- नॉर्वे:
- नॉर्वे में भी जमानत की प्रक्रिया कोर्ट द्वारा नियंत्रित होती है।
- यहां जमानत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी की उपस्थिति न्यायालय में हो, और जमानत देने से पहले अपराध की गंभीरता और आरोपी की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
प्रश्न 202: भारत और ब्राजील में “Police Custody” (पुलिस हिरासत) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस हिरासत के तहत गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन यह “Criminal Procedure Code” के तहत सीमित समय के लिए होता है।
- पुलिस हिरासत में रखे जाने की अधिकतम अवधि 15 दिन है, और इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ब्राजील:
- ब्राजील में पुलिस हिरासत को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम हैं।
- यहां पुलिस हिरासत को केवल परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और आरोपी को जल्द से जल्द न्यायालय में पेश किया जाता है।
प्रश्न 203: भारत और चीन में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद के खिलाफ “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” के तहत कड़े प्रावधान हैं।
- इसमें आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष अदालतें और आतंकवादी संगठनों की निगरानी के उपाय हैं।
- चीन:
- चीन में आतंकवाद के खिलाफ “Anti-Terrorism Law” है, जिसमें कड़े उपाय और अभियोजन के प्रावधान हैं।
- चीन में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त दंड और निगरानी की प्रणाली है, और इस कानून के तहत आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं।
प्रश्न 204: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में “Extradition” (प्रत्यक्षीकरण) प्रक्रिया की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Extradition Act, 1962” के तहत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया होती है।
- भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों के आधार पर प्रत्यर्पण करता है, जिससे अपराधी को एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
- अमेरिका में प्रत्यर्पण प्रक्रिया “Extradition Treaty” पर आधारित है, जो अमेरिका और अन्य देशों के बीच होती है।
- प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कड़े कानूनों और समझौतों के तहत होती है।
प्रश्न 205: भारत और इजराइल में “Self-Incrimination” (स्वयं की साक्षात्कार) का सिद्धांत क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Article 20(3) of the Constitution” के तहत स्वयं के खिलाफ गवाही देने से इंकार करने का अधिकार दिया गया है।
- आरोपी को यह अधिकार है कि वह स्वयं के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दे सकता।
- इजराइल:
- इजराइल में भी “Self-Incrimination” का सिद्धांत है, और यहां भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने से इंकार करने का अधिकार है।
- इस अधिकार का पालन इजराइली आपराधिक कानून और संविधान द्वारा किया जाता है।
प्रश्न 206: भारत और न्यूजीलैंड में “Corruption Laws” (भ्रष्टाचार कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ “Prevention of Corruption Act, 1988” और “Central Bureau of Investigation” के तहत कार्रवाई की जाती है।
- सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और अभियोजन की व्यवस्था है।
- न्यूजीलैंड:
- न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ “Crimes Act, 1961” और “Secret Commissions Act, 1910” के तहत सख्त कानून हैं।
- यहां भी सरकारी और निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 207: भारत और पाकिस्तान में “Habeas Corpus” (हैबियस कॉर्पस) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Habeas Corpus” का अधिकार संविधान में निहित है, और यह किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है।
- यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह “Habeas Corpus” याचिका दाखिल कर सकता है।
- पाकिस्तान:
- पाकिस्तान में भी “Habeas Corpus” का अधिकार संविधान में है, और यह अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने की सुविधा प्रदान करता है।
- पाकिस्तान में “Habeas Corpus” का उपयोग किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है।
प्रश्न 208: भारत और ब्रिटेन में “Police Accountability” (पुलिस जिम्मेदारी) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस की जिम्मेदारी “Police Act” और “Criminal Procedure Code” के तहत तय की जाती है।
- पुलिस अधिकारियों के कृत्य की निगरानी के लिए विभिन्न समितियां और आयोग होते हैं, जैसे कि “National Human Rights Commission”।
- ब्रिटेन:
- ब्रिटेन में पुलिस की जिम्मेदारी “Police and Crime Commissioners” और “Independent Office for Police Conduct” द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
- यहां पुलिस अधिकारियों के कार्यों की निगरानी और जांच की व्यवस्था है, और यदि कोई अधिकारी गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
प्रश्न 209: भारत और स्वीडन में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में गवाह सुरक्षा के लिए “Witness Protection Scheme, 2018” का प्रावधान है।
- गवाहों को पहचान छिपाने, सुरक्षित स्थानों पर भेजने और अन्य सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
- स्वीडन:
- स्वीडन में गवाहों की सुरक्षा के लिए अलग से “Witness Protection Program” है।
- इसमें गवाहों को नई पहचान, सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना और अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रश्न 210: भारत और जर्मनी में “Juvenile Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” के तहत विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- इस कानून के तहत बाल अपराधियों को सजा के बजाय सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास की सुविधा दी जाती है।
- जर्मनी:
- जर्मनी में “Youth Criminal Law” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रिया है।
- जर्मनी में भी अपराधियों को सुधारात्मक उपायों और पुनर्वास के जरिए न्याय मिलता है।
यहां तुलनात्मक आपराधिक प्रक्रिया (Comparative Criminal Procedure) से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं:
प्रश्न 211: भारत और यूके में “Sentencing Procedure” (दंड प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में दंड प्रक्रिया “Indian Penal Code” और “Criminal Procedure Code” के तहत निर्धारित की जाती है।
- दंड में जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, जैसे कि हत्या और आतंकवाद से संबंधित अपराधों में।
- यूके:
- यूके में दंड प्रक्रिया “Criminal Justice Act” और अन्य संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित की जाती है।
- यहां दंड की व्यवस्था में जेल, सामुदायिक सेवा, और जुर्माना शामिल होते हैं। मृत्युदंड को 1965 में रद्द कर दिया गया था।
प्रश्न 212: भारत और स्पेन में “Right to Fair Trial” (न्यायपूर्ण परीक्षण का अधिकार) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Right to Fair Trial” संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण और पारदर्शी परीक्षण का अधिकार प्रदान करता है।
- यहां आरोपी को आरोपों का सामना करने, वकील नियुक्त करने और उचित समय पर सुनवाई का अधिकार मिलता है।
- स्पेन:
- स्पेन में भी “Right to Fair Trial” संविधान में है और यूरोपीय संघ के मानवाधिकार कानूनों के तहत यह सुनिश्चित किया गया है।
- स्पेन में यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई मिले।
प्रश्न 213: भारत और स्विट्जरलैंड में “Extradition Process” (प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया “Extradition Act, 1962” के तहत संचालित होती है।
- भारत विभिन्न देशों से प्रत्यर्पण के लिए द्विपक्षीय संधियों पर निर्भर रहता है, और यह प्रक्रिया न्यायालय और सरकार द्वारा नियंत्रित होती है।
- स्विट्जरलैंड:
- स्विट्जरलैंड में भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों पर आधारित होती है।
- यहां आरोपी को प्रत्यर्पित करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपराध दोनों देशों के कानूनों के तहत संगत हो।
प्रश्न 214: भारत और कनाडा में “Habeas Corpus” (हैबियस कॉर्पस) का अधिकार कैसे कार्य करता है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Habeas Corpus” का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत दिया गया है।
- इसका उद्देश्य अवैध रूप से गिरफ्तार या कैद किए गए व्यक्तियों को न्यायालय में पेश कराना है।
- कनाडा:
- कनाडा में भी “Habeas Corpus” का अधिकार “Canadian Charter of Rights and Freedoms” के तहत है।
- अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह न्यायालय में यह याचिका दाखिल कर सकता है।
प्रश्न 215: भारत और पाकिस्तान में “National Security Laws” (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानूनों में “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” और “National Security Act, 1980” शामिल हैं।
- ये कानून आतंकवाद, राष्ट्रद्रोह, और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बनाए गए हैं।
- पाकिस्तान:
- पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में “Anti-Terrorism Act, 1997” और “Pakistan Protection Ordinance, 2013” शामिल हैं।
- पाकिस्तान के इन कानूनों के तहत आतंकवाद, सशस्त्र विद्रोह और अन्य सुरक्षा खतरे से निपटा जाता है।
प्रश्न 216: भारत और ऑस्ट्रेलिया में “Juvenile Justice” (बाल अपराध न्याय) की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में बाल अपराधों के लिए “Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” लागू है।
- इस कानून के तहत बाल अपराधियों को सुधारात्मक उपायों के रूप में पुनर्वास और शिक्षा देने का प्रावधान है।
- ऑस्ट्रेलिया:
- ऑस्ट्रेलिया में बाल अपराध न्याय की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के कानून के तहत होती है, लेकिन सामान्य रूप से “Juvenile Justice Act” के तहत बाल अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक प्रक्रियाएं हैं।
- यहां भी अपराधियों को सजा की बजाय सुधारात्मक उपायों के रूप में रखा जाता है।
प्रश्न 217: भारत और फ्रांस में “Witness Protection” (गवाह सुरक्षा) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में “Witness Protection Scheme, 2018” के तहत गवाहों की सुरक्षा की जाती है।
- इसमें गवाहों को पहचान छिपाने, सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है।
- फ्रांस:
- फ्रांस में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक विशेष “Witness Protection Program” है।
- इसमें गवाहों को नए पहचान पत्र, सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा दी जाती है।
प्रश्न 218: भारत और स्वीडन में “Drug Laws” (नशीली दवाओं के कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी के खिलाफ “Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985” के तहत कड़े कानून हैं।
- इस कानून के तहत नशीली दवाओं की तस्करी और इसके उपयोग को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- स्वीडन:
- स्वीडन में नशीली दवाओं के खिलाफ “Narcotic Drugs Act” है, जो नशीली दवाओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- स्वीडन में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड और सुधारात्मक उपाय हैं।
प्रश्न 219: भारत और जर्मनी में “Police Accountability” (पुलिस जवाबदेही) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में पुलिस की जवाबदेही “Police Act” और “Criminal Procedure Code” के तहत निर्धारित होती है।
- पुलिस कृत्यों की निगरानी के लिए विभिन्न आयोग और समितियां काम करती हैं, जैसे “National Human Rights Commission” और “State Human Rights Commissions”।
- जर्मनी:
- जर्मनी में पुलिस की जवाबदेही “German Police Act” और “Federal Police Act” के तहत होती है।
- यहां पुलिस कृत्यों की निगरानी और जांच करने के लिए स्वतंत्र संस्थाएं और आयोग हैं।
प्रश्न 220: भारत और इटली में “Terrorism Laws” (आतंकवाद कानून) की स्थिति क्या है?
उत्तर:
- भारत:
- भारत में आतंकवाद के खिलाफ “Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967” और अन्य सुरक्षा कानून लागू हैं।
- आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी संगठनों और उनके फंडिंग पर कठोर कार्रवाई की जाती है।
- इटली:
- इटली में आतंकवाद से निपटने के लिए “Anti-Terrorism Laws” लागू हैं।
- इटली में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, और यह कानून यूरोपीय संघ के आतंकवाद विरोधी उपायों के अनुरूप है।