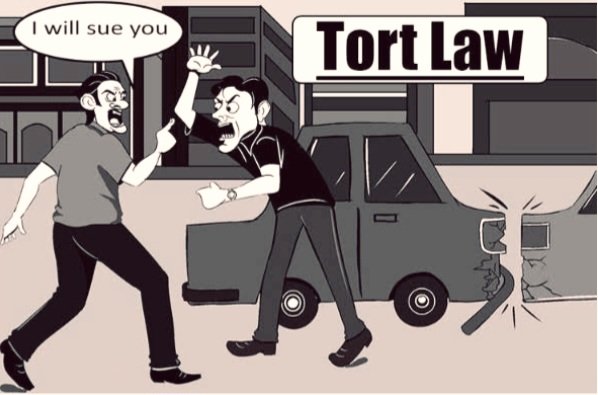लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर (Short Answer Type Questions)
1. अपकृत्य (दुष्कृति) का अर्थ (Meaning of Tort):
अपकृत्य (Tort) एक नागरिक (Civil) गलत कार्य है, जिसके लिए क्षतिपूर्ति (Compensation) का दावा किया जा सकता है। यह ऐसा कृत्य होता है जो किसी अन्य व्यक्ति को कानूनी क्षति पहुँचाता है और जिसके लिए नागरिक अदालत में उपचार (Remedy) उपलब्ध होता है।
2. अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of Tort):
- नागरिक गलत (Civil Wrong) – यह एक नागरिक अपराध होता है, न कि आपराधिक।
- निजी अधिकार का उल्लंघन (Violation of Private Rights) – यह किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है।
- कानूनी क्षतिपूर्ति (Legal Remedy) – पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
- कर्तव्य का उल्लंघन (Breach of Duty) – इसमें एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करता है।
3. अपकृत्य के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Tort):
- कर्तव्य का अस्तित्व (Existence of Duty) – एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कानूनी कर्तव्य होना चाहिए।
- कर्तव्य का उल्लंघन (Breach of Duty) – उक्त कर्तव्य का उल्लंघन हुआ हो।
- कानूनी क्षति (Legal Damage) – व्यक्ति को वास्तविक या संभावित क्षति हुई हो।
- क्षतिपूर्ति (Compensation) – प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का अधिकार हो।
4. अपकृत्य की प्रकृति (Nature of Tort):
- अपकृत्य असंविदानिक (Non-Contractual) गलत होता है।
- यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- यह सिविल लॉ का हिस्सा है, न कि क्रिमिनल लॉ।
- इसमें अदालत क्षतिपूर्ति (Damages) का आदेश दे सकती है।
5. “जहाँ उपचार है, वहीं अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है।” (Ubi Remedium Ibi Jus, Ubi Jus Ibi Remedium):
इस सूक्ति का अर्थ है कि यदि कोई अधिकार (Right) दिया गया है, तो उसके संरक्षण के लिए उपचार (Remedy) भी उपलब्ध होगा। इसी तरह, यदि कोई उपचार (Remedy) है, तो इसका मतलब है कि कोई अधिकार (Right) भी होना चाहिए।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसे कानूनी रूप से क्षतिपूर्ति (Compensation) प्राप्त करने का अधिकार होगा।
6. अपकृत्य एवं अपराध में भेद (Difference between Tort and Crime):
अपकृत्य (Tort) और अपराध (Crime) में मुख्य रूप से कई अंतर होते हैं। अपकृत्य एक नागरिक (सिविल) गलत कार्य होता है, जबकि अपराध एक आपराधिक (क्रिमिनल) कृत्य होता है। अपकृत्य किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके लिए प्रभावित व्यक्ति क्षतिपूर्ति (Compensation) का दावा कर सकता है। दूसरी ओर, अपराध समाज के विरुद्ध किया गया कार्य होता है और इसमें सरकार अपराधी को दंडित करती है।
अपकृत्य के मामलों में पीड़ित पक्ष स्वयं मुकदमा करता है और न्यायालय द्वारा हर्जाना दिया जाता है, जबकि अपराध में सरकार अभियोजन पक्ष होती है और दोषी को दंड दिया जाता है, जैसे जुर्माना या कारावास। अपराध का उद्देश्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है, जबकि अपकृत्य का उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को नुकसान की भरपाई दिलाना होता है।
उदाहरण के रूप में, मानहानि (Defamation) या संपत्ति में अतिक्रमण (Trespass) अपकृत्य हो सकते हैं, जबकि चोरी (Theft) और हत्या (Murder) अपराध होते हैं।
7. “प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता।” (Every Civil Wrong is not Tort):
हर नागरिक गलत कार्य को अपकृत्य नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, अनुबंध (Contract) के उल्लंघन को अनुबंध कानून (Contract Law) के अंतर्गत देखा जाता है, न कि अपकृत्य के रूप में।
8. विधि की भूल (Mistake of Law):
यदि कोई व्यक्ति किसी कानून की जानकारी न होने के कारण कोई गलत कार्य करता है, तो उसे विधि की भूल (Mistake of Law) कहा जाता है। यह एक सामान्य नियम है कि “कानून की अज्ञानता (Ignorance of Law) किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकती।”
9. बिना हानि के क्षति (Injuria Sine Damnum):
इसका अर्थ है कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, भले ही वास्तविक नुकसान न हुआ हो।
उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति को वोट देने से रोका जाता है, तो यह उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन है, भले ही उसे कोई आर्थिक हानि न हुई हो।
10. बिना क्षति के हानि (Damnum Sine Injuria):
इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को हानि हुई हो, लेकिन कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो।
उदाहरण: यदि कोई नया व्यवसाय खुलने से पुराने व्यवसाय की आय घट जाती है, तो यह आर्थिक हानि है, लेकिन यह अपकृत्य नहीं है।
11. अपकृत्य एवं नैतिक अपराध में अन्तर (Difference between Tort and Moral Crime):
- अपकृत्य कानून द्वारा परिभाषित होता है और इसका उपचार कानूनी प्रक्रिया से होता है।
- नैतिक अपराध समाज की नैतिकता पर आधारित होता है और इसका कानूनी उपचार आवश्यक नहीं होता।
12. कानूनी या विधिक क्षति (Legal Injury):
जब किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, भले ही उसे कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो, तो इसे कानूनी क्षति (Legal Injury) कहा जाता है।
उदाहरण:
- किसी व्यक्ति को पार्क में प्रवेश करने से रोका जाना, जबकि उसके पास वैध अनुमति हो।
- मानहानि का आरोप, भले ही आर्थिक हानि न हुई हो।
13. संयुक्त अपकृत्यकर्ता (Joint Tort-Feasors) से आप क्या समझते हैं?
जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता (Joint Tort-Feasors) कहा जाता है। वे सभी एक साथ या अलग-अलग उत्तरदायी हो सकते हैं, और पीड़ित व्यक्ति किसी एक या सभी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
14. प्रतिनिहित दायित्व (Vicarious Liability) से आप क्या समझते हैं?
यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपकृत्य न करते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है।
उदाहरण:
- नियोक्ता (Employer) अपने कर्मचारी (Employee) द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
- मालिक (Master) अपने सेवक (Servant) के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
15. गर्भस्थ शिशु (Child in Womb):
गर्भ में स्थित शिशु को गर्भस्थ शिशु कहा जाता है। कानून में कुछ स्थितियों में गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को भी मान्यता दी जाती है, जैसे उत्तराधिकार के मामलों में जन्म के बाद अधिकार प्राप्त करना।
16. आत्म-सुरक्षा (Self Defence):
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन, संपत्ति या स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग करता है, तो इसे आत्म-सुरक्षा कहा जाता है। यह एक कानूनी प्रतिरक्षा (Legal Defense) है, जिससे व्यक्ति पर कोई उत्तरदायित्व नहीं आता।
17. क्षति की दूरवर्तिता का सिद्धांत (Doctrine of Remoteness):
यह सिद्धांत कहता है कि केवल वही क्षति (Damage) कानूनन मान्य होगी, जो प्रत्यक्ष और पूर्वानुमेय (Foreseeable) हो। बहुत दूर की या अप्रत्याशित क्षति के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा।
उदाहरण: यदि किसी सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल होता है और कई दिनों बाद किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के लिए दुर्घटना करने वाला उत्तरदायी नहीं होगा।
18. “सहमति से क्षति नहीं होती” (Volenti non fit Injuria):
इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी जोखिम (Risk) को स्वीकार करता है, तो वह बाद में हानि के लिए दावा नहीं कर सकता।
उदाहरण: खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी चोट के लिए आयोजनकर्ताओं पर दावा नहीं कर सकते, यदि उन्होंने स्वेच्छा से भाग लिया हो।
19. राज्य कृत्य (Acts of State) से आप क्या समझते हैं?
राज्य द्वारा किए गए ऐसे कार्य, जो उसकी संप्रभुता (Sovereignty) के अंतर्गत आते हैं और जिन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, उन्हें राज्य कृत्य कहा जाता है।
उदाहरण: युद्ध, विदेशी संधियाँ, या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय।
20. हेतु (Motive) से आप क्या समझते हैं?
हेतु वह उद्देश्य (Intention) होता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। हालांकि, अपकृत्य के मामलों में हेतु (Motive) आमतौर पर महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि क्या कोई कानूनी हानि हुई है या नहीं।
21. क्षति एवं क्षतिपूर्ति (Damage and Damages):
क्षति (Damage): किसी व्यक्ति को हुआ वास्तविक नुकसान।
क्षतिपूर्ति (Damages): न्यायालय द्वारा दी गई आर्थिक भरपाई, जो पीड़ित व्यक्ति को नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है।
22. अवश्यम्भावी घटनाएँ (Inevitable Accidents) क्या हैं?
वे घटनाएँ, जिन्हें कोई भी सावधानी बरतने के बाद भी रोका नहीं जा सकता, अवश्यम्भावी घटनाएँ कहलाती हैं।
उदाहरण: अचानक आई प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप या बाढ़, जो किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती।
23. अपकृत्य विधि के लिए न्यायिक उपचार (Judicial Remedies of Torts):
- क्षतिपूर्ति (Damages): न्यायालय द्वारा हानि की भरपाई के लिए दी गई धनराशि।
- निषेधाज्ञा (Injunction): किसी कार्य को रोकने के लिए दिया गया आदेश।
- पुनर्स्थापन (Restitution): स्थिति को पहले जैसी बहाल करना।
24. हमला (Assault) को परिभाषित कीजिए।
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार धमकाता है कि वह वास्तविक शारीरिक हानि की संभावना से डर जाए, तो उसे हमला (Assault) कहा जाता है।
उदाहरण: किसी को डराने के लिए हथियार दिखाना, भले ही हमला न किया गया हो।
25. प्रहार (Battery) को समझाइए।
जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को अवांछित रूप से स्पर्श करता है या चोट पहुँचाता है, तो उसे प्रहार (Battery) कहा जाता है।
उदाहरण: किसी को बिना उसकी सहमति के थप्पड़ मारना।
26. प्रहार (Battery) तथा संप्रहार (Assault) में अंतर:
- संप्रहार (Assault) सिर्फ धमकी होती है, जिसमें शारीरिक संपर्क नहीं होता।
- प्रहार (Battery) में वास्तविक शारीरिक संपर्क होता है।
उदाहरण: - किसी को घूंसा मारने के लिए हाथ उठाना (Assault)
- वास्तव में घूंसा मार देना (Battery)
27. ‘मिथ्या कारावास’ (False Imprisonment) से आप क्या समझते हैं?
जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है या उसकी स्वतंत्रता पर बिना वैध कारण के रोक लगाई जाती है, तो उसे मिथ्या कारावास (False Imprisonment) कहा जाता है।
उदाहरण: किसी व्यक्ति को बिना कानूनी अधिकार के एक कमरे में बंद कर देना।
28. अचल सम्पत्ति के प्रति अपकृत्य (Torts Relating to Immovable Property):
वे अपकृत्य जो किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति (जैसे भूमि, भवन) से संबंधित होते हैं, उन्हें अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य कहा जाता है।
उदाहरण:
- अतिचार (Trespass to Land): किसी की भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश करना।
- उपद्रव (Nuisance): किसी व्यक्ति के भूमि उपयोग में बाधा डालना, जैसे धुआं, शोर या प्रदूषण।
29. चल संपत्ति के प्रति अपकृत्य (Torts Relating to Movable Property):
वे अपकृत्य जो किसी की चल संपत्ति (Movable Property) से संबंधित होते हैं।
उदाहरण:
- सम्परिवर्तन (Conversion): किसी की वस्तु को अवैध रूप से अपने पास रखना या उसे नुकसान पहुँचाना।
- चल संपत्ति का अतिचार (Trespass to Goods): किसी की संपत्ति को बिना अनुमति के छूना, ले जाना या नुकसान पहुँचाना।
30. आरम्भतः अतिचार (Trespass Ab Initio) से आप क्या समझते हैं?
जब कोई व्यक्ति कानूनन किसी संपत्ति में प्रवेश करता है, लेकिन बाद में उसका उपयोग अवैध रूप से करता है, तो उसे Trespass ab initio कहा जाता है।
उदाहरण: पुलिस किसी कानूनी वारंट के तहत प्रवेश करती है, लेकिन बाद में गैरकानूनी रूप से संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है।
31. सम्परिवर्तन (Conversion) क्या है?
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की चल संपत्ति का स्वामित्व अवैध रूप से अपने पास रख लेता है या उसे नष्ट कर देता है, तो इसे सम्परिवर्तन (Conversion) कहते हैं।
उदाहरण: किसी की कार को बिना अनुमति के उपयोग करना और उसे बेच देना।
32. उपेक्षा या असावधानी (Negligence) से आप क्या समझते हैं?
जब कोई व्यक्ति कानूनी कर्तव्य (Duty of Care) का पालन नहीं करता और इसके कारण किसी अन्य को हानि होती है, तो इसे उपेक्षा (Negligence) कहते हैं।
उदाहरण: डॉक्टर की लापरवाही से गलत दवा देना।
33. विद्वेष (Malice):
विद्वेष का अर्थ है किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की मंशा। यह अपकृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उदाहरण: झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना।
34. उपताप (Nuisance) क्या है?
जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का उचित उपयोग करने से वंचित करता है, तो इसे उपताप (Nuisance) कहते हैं।
उदाहरण: शोर प्रदूषण, दुर्गंध फैलाना, अनावश्यक रोशनी फैलाना।
35. सार्वजनिक उपताप (Public Nuisance) से आप क्या समझते हैं?
सार्वजनिक उपताप तब होता है जब किसी व्यक्ति का कार्य संपूर्ण समाज या जनता को प्रभावित करता है।
उदाहरण: अवैध रूप से सड़क पर बाधा खड़ी करना, नदी को प्रदूषित करना।
36. निजी उपताप (Private Nuisance) और सार्वजनिक उपताप (Public Nuisance) में अंतर:
- निजी उपताप: जब किसी व्यक्ति की संपत्ति या अधिकार पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ता है।
- सार्वजनिक उपताप: जब संपूर्ण समाज या बड़े समूह को नुकसान होता है।
उदाहरण: - पड़ोसी का अत्यधिक तेज़ संगीत बजाना (Private Nuisance)।
- सार्वजनिक सड़क पर कूड़ा फेंकना जिससे यातायात बाधित हो (Public Nuisance)।
37. योगदायी उपेक्षा (Contributory Negligence) क्या है?
जब किसी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की भी कुछ हद तक गलती होती है, तो इसे योगदायी उपेक्षा कहते हैं।
उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और दुर्घटना हो जाती है, तो उसे भी आंशिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
38. कठोर दायित्व (Strict Liability) पर संक्षिप्त टिप्पणी:
इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति खतरनाक गतिविधि करता है और उससे किसी को हानि होती है, तो भले ही उसने कोई लापरवाही न की हो, फिर भी वह उत्तरदायी होगा।
उदाहरण: किसी कारखाने से रासायनिक गैस लीक होने पर मालिक उत्तरदायी होगा।
39. पूर्ण दायित्व (Absolute Liability) की व्याख्या कीजिए।
पूर्ण दायित्व कठोर दायित्व का एक उन्नत रूप है, जिसमें कोई अपवाद (Exception) नहीं होता।
उदाहरण: MC Mehta v. Union of India (1987), जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के लिए कंपनी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।
40. षड्यंत्र (Conspiracy) क्या है?
जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अन्य को नुकसान पहुँचाने के लिए एक साथ योजना बनाते हैं, तो इसे षड्यंत्र (Conspiracy) कहते हैं।
उदाहरण: किसी व्यापारी को व्यापार से बाहर करने के लिए प्रतिस्पर्धी व्यापारियों का मिलकर साजिश रचना।
41. आवश्यकता (Necessity) क्या है?
आवश्यकता एक कानूनी बचाव (Legal Defense) है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए कानून का उल्लंघन करता है।
उदाहरण: यदि किसी जलते हुए घर में प्रवेश करके किसी को बचाया जाता है, तो यह आवश्यकता के अंतर्गत आएगा।
42. अवयस्क (Minor):
एक अवयस्क वह व्यक्ति होता है, जिसकी आयु अभी तक कानूनी वयस्कता की सीमा तक नहीं पहुँची है। भारत में, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क माना जाता है।
43. सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority):
जब कोई कार्य किसी विशेष क़ानून या अधिनियम द्वारा अधिकृत (Authorized) होता है, तो उसे सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority) कहा जाता है। यह एक पूर्ण प्रतिरक्षा (Absolute Defense) के रूप में कार्य करता है।
उदाहरण: नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण कार्य करने से होने वाली असुविधा के लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता।
44. मानहानि (Defamation) से क्या तात्पर्य है?
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने वाला झूठा कथन (False Statement) प्रकाशित करता है या सार्वजनिक रूप से कहता है, तो इसे मानहानि (Defamation) कहते हैं।
मुख्य प्रकार:
- अपवचन (Slander): अस्थायी रूप से बोले गए शब्दों द्वारा मानहानि।
- अपकथन (Libel): स्थायी रूप से लिखित, मुद्रित, या चित्रों द्वारा की गई मानहानि।
45. वक्रोक्ति (Innuendo):
जब कोई कथन सीधे तौर पर अपमानजनक न हो, लेकिन उसमें छिपा हुआ अर्थ (Hidden Meaning) किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए, तो इसे वक्रोक्ति (Innuendo) कहा जाता है।
उदाहरण: “वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है… जब तक उसे मौका न मिले!”
46. अपवचन (Slander):
जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने के लिए मौखिक रूप से झूठे और अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं, तो इसे अपवचन (Slander) कहते हैं।
47. अपकथन (Libel):
जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने के लिए लिखित, मुद्रित, या चित्रों द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो इसे अपकथन (Libel) कहते हैं।
उदाहरण: अखबार में झूठी अफवाहें प्रकाशित करना।
48. विद्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution):
जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करता है, तो इसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन (Malicious Prosecution) कहा जाता है।
49. अतिचार (Trespass):
जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी की संपत्ति, भूमि, या शरीर पर हस्तक्षेप करता है, तो इसे अतिचार (Trespass) कहा जाता है।
प्रकार:
- भूमि पर अतिचार (Trespass to Land)
- संपत्ति पर अतिचार (Trespass to Goods)
- व्यक्ति पर अतिचार (Trespass to Person)
50. “अन्तिम अवसर का सिद्धांत” (Last Opportunity Rule):
यह सिद्धांत कहता है कि जब एक दुर्घटना में दोनों पक्षों की गलती हो, तो वह पक्ष अधिक उत्तरदायी होगा, जिसे अंतिम अवसर (Last Opportunity) था नुकसान को रोकने का।
51. “दैवी कृत्य” (Act of God) को परिभाषित कीजिए।
जब कोई प्राकृतिक आपदा (जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान) किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है और इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, तो इसे दैवी कृत्य (Act of God) कहा जाता है।
उदाहरण: भूकंप से मकान गिरना, जिसे कोई रोक नहीं सकता।
52. ‘घटना स्वयं प्रमाण है’ (Res Ipsa Loquitur) का सिद्धांत क्या है?
इस सिद्धांत का अर्थ है कि “घटना स्वयं ही अपने लिए बोलती है।” जब किसी घटना में लापरवाही इतनी स्पष्ट होती है कि इसे साबित करने के लिए अलग से साक्ष्य की जरूरत नहीं होती।
उदाहरण: अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर द्वारा मरीज के शरीर में औजार छोड़ देना।
53. मानसिक आघात (Nervous Shock) के लिए क्षतिपूर्ति:
यदि किसी व्यक्ति को किसी घटना के कारण मानसिक तनाव या सदमा (Mental Shock) पहुँचता है, तो उसे मानसिक आघात (Nervous Shock) कहा जाता है, और वह क्षतिपूर्ति का हकदार हो सकता है।
उदाहरण: किसी प्रियजन की दुर्घटना देखने के बाद मानसिक तनाव का शिकार होना।
54. मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के लिए प्रतिकर के दावा का अधिकार:
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, तो उसके परिवार को मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे (Compensation) का अधिकार होता है।
55. ‘दोष-रहित दायित्व’ (No Fault Liability) की व्याख्या करें (Motor Vehicles Act, 1988):
इस सिद्धांत के अनुसार, यदि सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु या चोट होती है, तो वाहन चालक को दोष साबित किए बिना ही मुआवजा देना होगा।
56. ‘उपभोक्ता’ (Consumer) को परिभाषित कीजिए।
उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, जो किसी वस्तु या सेवा को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदता है।
उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति बाज़ार से टीवी खरीदता है और उसमें खराबी होती है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।
57. उपभोक्ता विवाद (Consumer Dispute):
जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से संबंधित त्रुटि, खराबी, अनुचित व्यवहार या धोखाधड़ी के कारण उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करता है, तो इसे उपभोक्ता विवाद (Consumer Dispute) कहा जाता है।
उदाहरण: किसी ग्राहक को घटिया गुणवत्ता का मोबाइल फोन दिया जाए और विक्रेता उसे बदलने से इनकार करे।
58. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (Central Consumer Protection Council) का गठन:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया गया है।
- यह एक सलाहकार निकाय (Advisory Body) है।
- इसके अध्यक्ष भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्री होते हैं।
- इसमें विभिन्न उद्योग, उपभोक्ता संघ, और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और नीतियाँ बनाने में सहयोग करना है।
59. जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum):
यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक न्यायालय (Court) है, जो जिला स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई करता है।
- यह 20 लाख रुपये तक के विवादों को हल करता है।
- अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं।
- यदि ग्राहक इस न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
60. उपभोक्तावाद (Consumerism) क्या है?
उपभोक्तावाद एक सामाजिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है।
मुख्य उपभोक्ता अधिकार:
- गुणवत्ता और सुरक्षा का अधिकार
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार
- पसंद करने का अधिकार
- शिकायत करने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
61. परिवाद (Complaint) से क्या समझते हैं?
जब कोई उपभोक्ता किसी त्रुटिपूर्ण उत्पाद या सेवा, अनुचित व्यापार व्यवहार, अधिकारों के उल्लंघन या धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज करता है, तो इसे परिवाद (Complaint) कहते हैं।
उदाहरण: कोई उपभोक्ता खराब टेलीविजन के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है।
62. अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) क्या है?
जब कोई व्यापारी या कंपनी ग्राहकों को धोखा देने, गुमराह करने या अनुचित तरीके से मुनाफा कमाने के लिए गलत व्यापारिक प्रथाओं का उपयोग करती है, तो इसे अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) कहते हैं।
उदाहरण:
- झूठे विज्ञापन देना (Fake Advertisement)
- उत्पाद की गलत जानकारी देना (Misleading Information)
- अधिक कीमत वसूलना (Overcharging)
- नकली उत्पाद बेचना (Selling Fake Products)
63. समस्याएँ (Problems) से क्या तात्पर्य है?
कानूनी दृष्टि से, समस्याएँ उन परिस्थितियों को दर्शाती हैं, जो व्यक्ति, समाज, व्यापार या कानून से संबंधित बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित समस्याएँ:
- नकली और मिलावटी उत्पादों की बिक्री।
- ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूली।
- खराब गुणवत्ता के सामान की आपूर्ति।
- ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी।
- शिकायतों के निवारण में देरी।