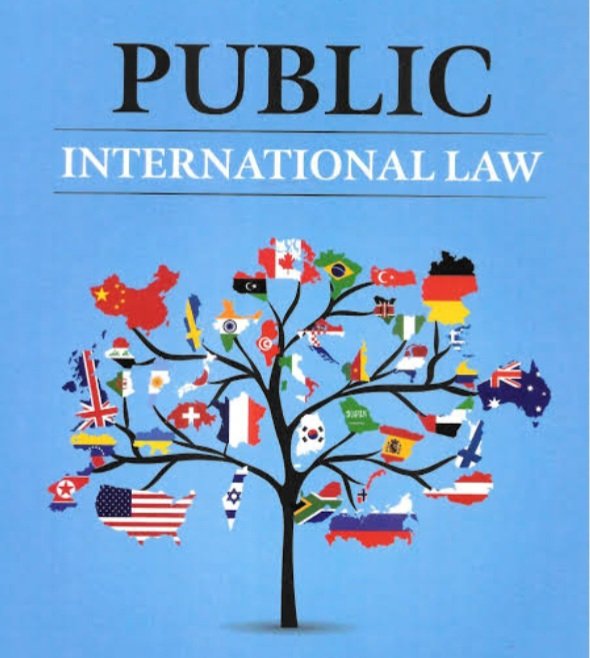Here are the answers to your questions:
- अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय विधि वह नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, और व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह वैश्विक स्तर पर विधिक अनुशासन के रूप में कार्य करता है।
- ऑस्टिन के विचार से सहमति: ऑस्टिन का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल “सकारात्मक नैतिकता” है, जिसे मैं असहमत हूं। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य के कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है, यह केवल नैतिक मार्गदर्शन नहीं होता।
- “अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिन्दु है”: यह विचार अंतर्राष्ट्रीय विधि के पारंपरिक रूप को समाप्त कर राष्ट्रीय कानूनों से अधिक स्वतंत्रता देने का संकेत करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि अब एक सशक्त न्यायिक प्रणाली में बदलने की ओर बढ़ रही है।
- क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है?: यह विचार विवादास्पद है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रभाव और कार्यान्वयन राष्ट्रीय विधियों के मुकाबले कमजोर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय निर्णयकर्ता नहीं होता।
- लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर: लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तिगत पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय कौन है? राज्य या व्यक्ति अथवा दोनों?: अंतर्राष्ट्रीय विधि का पारंपरिक विषय राज्य है, लेकिन अब व्यक्ति भी महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं, खासकर मानवाधिकारों और युद्ध अपराधों के मामले में।
- पैक्टा सन्ट सर्वेन्डा: यह सिद्धांत कहता है कि संधियों को निष्पक्षता से सम्मानित किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए।
- संधियों का वर्णन किस अभिसमय में किया गया है?: संधियों का वर्णन “विएना संधि विधि सम्मेलन 1969” में किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत हैं: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय, और अंतर्राष्ट्रीय परंपरा।
Here are the answers to your questions:
- “सन्धियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत के रूप में”: संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि जब राज्य या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ संधि पर हस्ताक्षर करती हैं, तो वे उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी मानते हैं। संधियाँ वैधानिक रूप से नियमों और कर्तव्यों को स्थापित करती हैं, जो सभी पक्षों के लिए लागू होते हैं।
- ‘रूढ़ि’ (Custom) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कुछ समय तक स्थापित होने पर वह ‘रूढ़ि’ (कस्टम) के रूप में विकसित होता है। यह एक प्रकार का परंपरागत कानून है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य तौर पर स्वीकृत और पालन किया जाता है।
- Ex acquo et bono: यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “समानता और भलाई के आधार पर”। इसका प्रयोग तब होता है जब एक न्यायालय किसी विवाद का निपटारा न्यायसंगत और मानवाधिकारों के सम्मान के आधार पर करता है।
- क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है?: अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विशिष्ट कानूनी ढांचा है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय विधियों की तरह सख्त कानूनी प्रवर्तन तंत्र नहीं होता। इसलिए इसे “सच्चे अर्थों में विधि” मानने पर संदेह हो सकता है, लेकिन यह एक प्रभावी विधिक अनुशासन है।
- भारत के अभ्यास के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के संबंध में: भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच एक दोहरा संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(c) में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान और उसकी दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ भारत में संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही लागू होती हैं।
- क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत होते हैं?: संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का कानूनी स्रोत नहीं होते, क्योंकि ये संकल्प गैर-बाध्यकारी होते हैं। हालांकि, जब ये संकल्प व्यापक स्वीकृति प्राप्त करते हैं, तो यह रूढ़ि (customary international law) का हिस्सा बन सकते हैं।
- ‘मान्यता’ (Recognition): मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है जिसमें एक राज्य, संगठन या राजनीतिक सत्ता अन्य राज्य या सत्ता को कानूनी रूप से पहचानता है। यह सामान्यतः किसी नए राज्य की स्थापना या किसी नई सरकार के मान्यता प्राप्त होने के संदर्भ में होता है।
- राष्ट्रीयता: राष्ट्रीयता उस कानूनी संबंध को कहा जाता है जो एक व्यक्ति को एक विशेष राज्य से जोड़ता है और उसे उस राज्य के अधिकार और कर्तव्यों से बाँधता है। यह उस व्यक्ति की नागरिकता को दर्शाती है।
- दोहरी आपराधिकता का सिद्धान्त: यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जा सकता है जो अपराध दोनों देशों के लिए कानूनन अपराध हो।
- (क) मान्यता के प्रकार:
- राजनीतिक मान्यता: किसी नए सरकार या राज्य को अन्य देशों द्वारा स्वीकार किया जाना।
- कानूनी मान्यता: किसी नए राज्य या सरकार को कानूनी रूप से अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होना।
(ख) विधिक मान्यता और तथ्येन मान्यता में अंतर:
- विधिक मान्यता: जब किसी राज्य या सरकार को कानूनी रूप से एक वैध इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- तथ्येन मान्यता: जब केवल राजनीतिक या वास्तविक स्थिति के आधार पर किसी राज्य या सरकार को स्वीकार किया जाता है, न कि कानूनी रूप से।
Here are the answers to your questions:
- अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ‘मान्यता’ के प्रभाव: मान्यता के प्रभावों में यह शामिल है कि जब एक राज्य या सरकार को मान्यता प्राप्त होती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कानूनी अधिकार प्राप्त करता है, जैसे कि संधियाँ करने का अधिकार, न्यायालयों में मुकदमा करने का अधिकार, और अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
- क्या मान्यता प्रदान करना राजनीतिक कार्य है?: हाँ, मान्यता एक राजनीतिक कार्य है, क्योंकि यह किसी राज्य या सरकार की वैधता और अस्तित्व को स्वीकार करने का निर्णय है, जो आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति पर निर्भर करता है।
- प्रत्यर्पण की आवश्यक शर्तें: प्रत्यर्पण उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें एक देश दूसरे देश को अपराधी को सौंपता है, ताकि उस पर वहाँ के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके। इसके आवश्यक शर्तों में अपराध का होने वाले देश और प्राप्त करने वाले देश के बीच प्रत्यर्पण समझौता होना चाहिए, अपराध दोनों देशों में अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और प्रत्यर्पण की शर्तों का पालन किया जाए।
- ‘प्रत्यर्पण’ से आप क्या समझते हैं? प्रत्यर्पण हेतु मान्य अधिकारों की विवेचना कीजिए: प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य किसी अन्य राज्य को उस अपराधी को सौंपता है, जो वहां अपराध करने के आरोप में वांछित होता है। इसके लिए अपराध दोनों देशों में समान होना चाहिए, और प्रत्यर्पण समझौते का अस्तित्व होना चाहिए।
- शरण को परिभाषित कीजिए: शरण किसी व्यक्ति को उसके देश से बाहर सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति है, जब वह अपनी जान, स्वतंत्रता, या मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए किसी अन्य देश में शरण लेता है।
- शरणार्थियों को ‘पुनः अस्थिर न करना’ सिद्धान्त: यह सिद्धांत यह कहता है कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उनके साथ अत्याचार, उत्पीड़न, या मौत का खतरा हो। इसे “Non-refoulement” कहा जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी अधिकारों का मूल सिद्धांत है।
- शरण और प्रत्यर्पण में अंतर:
- शरण: यह सुरक्षा का अधिकार है, जिसे एक व्यक्ति एक दूसरे देश से प्राप्त करता है, जब उसे अपने देश में उत्पीड़न का खतरा हो।
- प्रत्यर्पण: यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक देश दूसरे देश को अपराधी को सौंपता है, ताकि उस पर अभियोग चलाया जा सके।
- (A) अंतर्राष्ट्रीय संधि की परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय संधि एक लिखित समझौता है जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।
(ख) रिबस सिक स्टैंटिबस: यह लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है “जब परिस्थितियाँ जैसी थीं वैसी बनी रहती हैं”। इसका उपयोग संधि के निषेध को समाप्त करने के लिए किया जाता है जब संबंधित परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। - (A) संधि का अंत: संधि का अंत तब होता है जब उसके लागू होने की अवधि समाप्त हो जाती है, या जब दोनों पक्ष एक-दूसरे से सहमति से इसे समाप्त कर देते हैं।
(B) संधियों का अनुसमर्थन: अनुसमर्थन एक प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य किसी संधि को स्वीकार करता है और इसे अपने देश में लागू करता है। यह संधि पर हस्ताक्षर के बाद होता है। - हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं?: हस्तक्षेप का मतलब है किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में बिना अनुमति के दखल देना। यह सामान्यतः राजनीतिक, सैन्य, या कूटनीतिक रूप में होता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादास्पद होता है।
Here are the answers to your questions:
- राजनयिक प्रतिनिधियों की परिभाषा: राजनयिक प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य में आधिकारिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। ये व्यक्ति आमतौर पर दूतावासों में कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शामिल होते हैं।
- राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्तियाँ एवं विशेषताएँ: राजनयिक अभिकर्ताओं को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि:
- राजनयिक छूट: वे उस देश के कानूनी क्षेत्राधिकार से मुक्त होते हैं, जहाँ वे काम करते हैं।
- कानूनी प्रतिरक्षा: उन्हें अपराधों के लिए न्यायिक कार्यवाही से छूट होती है।
- करों से छूट: वे राजनयिक कार्यों से संबंधित कुछ करों से मुक्त होते हैं।
- संपत्ति की सुरक्षा: उनके निजी और आधिकारिक स्थानों की सुरक्षा होती है।
- राज्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?: राज्य क्षेत्र से तात्पर्य उस भू-भाग से है जो एक राज्य के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसमें स्थल, जल, वायुमंडल और उपभोक्तीय संसाधन शामिल हैं।
- प्रादेशिक आश्रय: प्रादेशिक आश्रय वह स्थिति है जब एक राज्य किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में शरण प्रदान करता है, विशेष रूप से जब वह व्यक्ति अपने देश में उत्पीड़न या अन्य प्रकार की आपत्ति से बचने के लिए वहां पहुंचता है।
- गैर-राज्य इकाइयाँ: गैर-राज्य इकाइयाँ वे संस्थाएँ होती हैं जो राज्यों के रूप में क़ानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन (NGOs), और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ।
- राज्य की अधिकारिता: राज्य की अधिकारिता (jurisdiction) उस राज्य के पास कानूनी अधिकार और शक्ति है, जिसके तहत वह अपने क्षेत्र के भीतर कानून लागू करता है, और अपने नागरिकों और अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकता है।
- राज्य उत्तराधिकार: राज्य उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसमें एक नया राज्य किसी पुराने राज्य के अधिकारों, कर्तव्यों और संपत्ति को प्राप्त करता है, विशेष रूप से जब कोई राज्य बदलता है या विघटित होता है।
- राज्य प्राप्त करने के मान्य तरीके: राज्य प्राप्त करने के मान्य तरीके में शामिल हैं:
- विजय (Conquest)
- विकास (Cession)
- संधि (Treaty)
- मुलायम क्षेत्रीय विस्तार (Effective occupation)
- सत्प्रयत्न: सत्प्रयत्न (Good Offices) वह प्रक्रिया है जिसमें एक तृतीय पक्ष दो संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान करता है, ताकि वे समझौते तक पहुंच सकें, लेकिन यह प्रक्रिया दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के बलपूर्वक तरीके: बलपूर्वक तरीके में युद्ध, सैन्य हस्तक्षेप, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा विवादों का समाधान शामिल हो सकते हैं, जब शांति साधनों से विवाद हल नहीं हो पाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के शान्तिपूर्वक तरीकों की संक्षेप में व्याख्या: शांति पूर्वक विवादों के निपटारे के तरीकों में बातचीत, मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक निर्णय और अन्य शांतिपूर्ण उपाय शामिल हैं, जो पक्षों को बिना हिंसा के समाधान तक पहुंचने में मदद करते हैं।
- ‘अंतरिक्ष विषयक अभिसमय’ क्या है?: ‘अंतरिक्ष विषयक अभिसमय’ (Convention on Outer Space) 1967 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम है, जो अंतरिक्ष के उपयोग और अन्वेषण से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, जिसमें अंतरिक्ष में हथियारों के प्रयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Here are the answers to your questions:
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और इसके महत्व:
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो मानवाधिकारों की बुनियादी मान्यताओं को पहचानता है और बताता है कि सभी व्यक्ति को समान और अविच्छिन्न अधिकार मिलते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, और सुरक्षा का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के। इसका महत्व इस तथ्य में है कि यह मानवाधिकारों को वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करता है, और यह देशों को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन मानव अधिकार:
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का स्पष्ट उद्देश्य है। चार्टर के अनुच्छेद 55 और 56 के तहत, यू.एन. सदस्य देशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे मानवाधिकारों का सम्मान करें और उन्हें बढ़ावा दें। इसके तहत विभिन्न कृत्य और उपायों के माध्यम से मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। - क्या आप इससे सहमत हैं कि मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है?
हां, मैं सहमत हूं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह न केवल मानवाधिकारों के वैश्विक मानकों की स्थापना करता है, बल्कि यह देशों को उनके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है। यू.एन. का मानवाधिकार परिषद, संबंधित संधियाँ और विभिन्न विशेष प्रक्रियाएँ इसकी भूमिका को मजबूत करती हैं। - बायुयान अपहरण:
बायुयान अपहरण (Aircraft Hijacking) एक अवैध कृत्य है, जिसमें कोई व्यक्ति विमान को नियंत्रित करता है और उसे जबरदस्ती एक निश्चित दिशा में ले जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, जिसे 1970 में हाग कंवेंशन द्वारा कानूनी रूप से परिभाषित किया गया था, और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर रूप से दंडनीय अपराध माना जाता है। - युद्धबन्दी के साथ व्यवहार:
युद्धबन्दी के साथ उचित और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जेनिवा कन्वेंशन 1949 के अनुच्छेद 3 के तहत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत युद्धबन्दियों को भेदभाव, यातना या अमानवीय व्यवहार से बचाया जाता है। उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान की जाती है, और उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता। - तटस्थता:
तटस्थता (Neutrality) वह स्थिति है जब कोई राज्य एक युद्ध में पक्ष नहीं लेता और किसी भी पक्ष को समर्थन या सहायता नहीं प्रदान करता। तटस्थता के तहत, तटस्थ देशों को युद्ध के दौरान अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा प्राप्त होती है और उन्हें संघर्ष के क़ानूनी प्रभावों से मुक्त रखा जाता है। - नाकाबन्दी:
नाकाबन्दी (Blockade) एक युद्ध कूटनीतिक या सैन्य उपाय है, जिसमें एक देश दूसरे देश के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों तक पहुँच को रोकता है। इसका उद्देश्य दुश्मन के व्यापार और आपूर्ति लाइनों को बाधित करना होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में निषिद्ध नहीं है, लेकिन इसे निष्पक्ष रूप से लागू करना आवश्यक होता है। - मानवाधिकारों की अवधारणा:
मानवाधिकारों की अवधारणा उस बुनियादी और स्वाभाविक अधिकारों की पहचान करती है जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, जीवन, और सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं और इनका उल्लंघन न करने का हर राज्य और समाज पर दायित्व होता है। - निषेधाधिकार की शक्ति:
निषेधाधिकार (Veto Power) वह शक्ति है जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, और फ्रांस) को दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि एक स्थायी सदस्य देश किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही अन्य सदस्य देशों का समर्थन हो। - नर-संहार:
नर-संहार (Genocide) एक अत्यंत गंभीर अपराध है, जिसमें किसी राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक, या जातीय समूह के सदस्यों को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामूहिक हत्या, उत्पीड़न, और शारीरिक या मानसिक नुकसान शामिल हो सकते हैं। यह अपराध 1948 के नरसंहार सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत परिभाषित किया गया है। - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद:
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं जो एक से अधिक देशों के नागरिकों, संगठनों, या सरकारी संस्थाओं को लक्षित करती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार अपराध, हिंसा, और आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है, और इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कृत्यों के द्वारा अपराध घोषित किया गया है। - आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत व्यक्ति के स्थान का परीक्षण:
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में, व्यक्ति को राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। आजकल, व्यक्ति केवल राज्य का विषय नहीं रहा, बल्कि उसे मानवीय अधिकारों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब, व्यक्ति को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में न्याय की मांग करने का अधिकार है, और उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मुकदमा दायर करने का अधिकार भी मिल सकता है। - युद्ध:
युद्ध एक कूटनीतिक, सैन्य, या वैचारिक संघर्ष है जिसमें दो या दो से अधिक राज्य या समूह एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में, युद्ध से संबंधित कई नियम और संधियाँ हैं, जैसे जेनिवा कन्वेंशन, जो युद्ध में मानवाधिकारों और युद्धबन्दियों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।