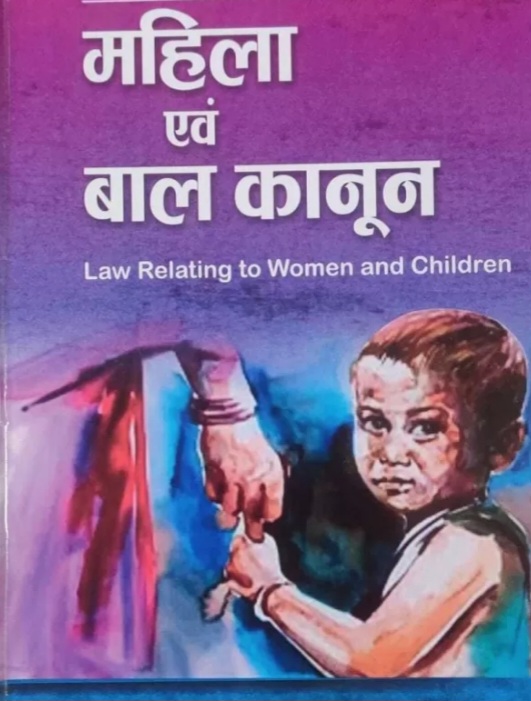अध्याय 4 महिलाओं का अशिष्ट रूपण
(Indecent Representation of Women)
प्रश्न 14. “महिलाओं के अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्रेत है? महिलाओं के अशिष्ट रूपण से सम्बन्धित अपराधों एवं इस पर प्रतिषेध का उल्लेख करें।
उत्तर- महिलाओं का अशिष्ट रूपण आज एक सामान्य बात हो गई है। महिलाओं को व्यावसायिक प्रचार का एक माध्यम बना दिया गया है। चाहे किसी भी चीज अथवा वस्तु का विज्ञापन हो, उसमें महिलाओं को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया जाता है, चाहे उस चीज अथवा वस्तु से महिलाओं का दूर-दूर तक सरोकार न हो।
इस प्रकार एक आदर्श नारी एवं कुशल गृहिणी कहलाने वाली महिला को आज व्यावसायिक प्रचार-प्रसार का माध्यम बना दिया गया है। व्यवसाय के प्रचार-प्रसार में चारों तरफ नारी ही नारी के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। साड़ियों से लगाकर सिगरेट तक, मंजन से लगाकर व्यंजन तक, वाहन से लगाकर वाईन तक नारी ही नारी के चित्र देखने में आते हैं। मॉडलिंग एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। मॉडलिंग में अंग प्रदर्शन एक सामान्य बात हो गई है। इतना ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में नारियों के अभद्र चित्र एवं अंग प्रदर्शित करते विज्ञापन बड़े चाव से छापे एवं पढ़े जाते हैं। बाजार में सेक्स विषयक साहित्य का अम्बार लगा हुआ है।
बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक और सिलसिला चल पड़ा है- सौन्दर्य प्रतियोगिताओं का। सौन्दर्य के नाम पर खुले आम मंच पर नारियों को अर्द्धनग्न अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। उनको अभद्र एवं अश्लील रूप में जनसाधारण के समक्ष पेश किया जाता है। महिलाओं की सौन्दर्य प्रतियोगितायें, न्यायालय में चुनौती का विषय भी बन चुकी हैं। इन सबके पश्चात् भी आज महिलाओं का अशिष्ट रूपण व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इसी के निवारण के लिए संसद द्वारा 1986 में “महिलाओं का अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम” पारित किया गया है।
अशिष्ट रूपण क्या है?
अधिनियम की धारा 2 (ग) में अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार महिलाओं के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय है-
“किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना, जिससे उसका चरित्र कलंकित होता हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अपदूषण अथवा अनैतिकता को हानि कारित होने की सम्भावना हो।”
विस्तृत भाव में यह कह सकते हैं कि स्त्री को इस रूप में प्रदर्शित करना जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो तथा जिससे जनसाधारण के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, अशिष्ट रूपण है।
किसी पुस्तक में नारी का ऐसा चित्रण अथवा रूपण किया जाना जिससे व्यक्ति में कामोत्तेजना बढ़ती हो अथवा चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, दण्डनीय अपराध है।
अशिष्ट रूपण का निषेध
अधिनियम की धारा 3 में महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का निषेध किया गया है।
धारा 4 में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले निम्नांकित के उत्पादन, विक्रय, वितरण आदि का निषेध किया गया है- पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण, चित्र आदि।
इनके परिचालन एवं डाक द्वारा प्रेषण को भी धारा 4 के अन्तर्गत निषेधित किया गया है।
इस विषय पर चन्द्रा राजकुमारी बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद, ए० आई० आर० (1998) आन्ध्र प्रदेश 302 का एक महत्वपूर्ण मामला है। यह महिलाओं की “सौन्दर्य प्रतियोगिता” से सम्बन्धित है। इस मामले में नारी के उच्च एवं आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि “नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं है अपितु एक शक्ति भी है। उसका नारीत्व माँ की ममता के रूप में छलकता है। ऐसी नारी का सम्मान एवं गौरव संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन संरक्षित है।”
सौन्दर्य का प्रदर्शन बुरा नहीं है। सौन्दर्य, प्रदर्शन योग्य भी है। लेकिन यदि उसका प्रदर्शन आपत्तिजनक रूप में किया गया है तो वही प्रदर्शन दण्डनीय अपराध बन जाता है।
इस मामले में “मिस आन्ध्र पर्सनालिटी कन्टेस्ट” को चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने इसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये, यथा-
(i) सौन्दर्य प्रतियोगिता में शालीनता एवं नारी गरिमा का ध्यान रखा जायेगा,
(ii) यह आन्ध्र प्रदेश की परम्परागत संस्कृति के अनुरूप होगी,
(iii) सौन्दर्य प्रतियोगिता के दौरान मादक एवं नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायेगा,
(iv) समुचित बैठक की व्यवस्था की जायेगी,
(v) प्रतियोगिता यथासम्भव रात्रि के 10 बजे पूर्व समाप्त हो जायेगी,
(vi) प्रतियोगिता का आयोजन एक उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में किया जायेगा, आदि।
निःसन्देह यह निर्णय महिलाओं के अशिष्ट रूपण को रोकने की दिशा में एक अहम निर्णय है। यह निर्णय सौन्दर्य प्रतियोगिता के व्यवसायीकरण पर प्रतिबन्ध लगाता है। नारी सम्मान की दिशा में इसे मील का पत्थर कहा जा सकता है।
शक्तियाँ
महिलाओं का अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम, 1986. की धारा 6 में शास्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति धारा 3 अथवा धारा 4 के अन्तर्गत महिलाओं के अशिष्ट रूपण का दोषी पाया जाता है तो उसे प्रथम अपराध के लिये दो वर्ष तक की अवधि के कारावास तथा दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
यदि कोई दोषसिद्ध व्यक्ति पुनः ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसे न्यूनतम छः माह के कारावास एवं अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के कारावास तथा न्यूनतम दस हजार रुपये के जुर्माने एवं अधिकतम एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
अध्याय 5
बाल विवाह/सती निवारण (Child Marriage/Prevention of Commission of Sati)
प्रश्न 15. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1929 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। अधिनियम के प्रभावी रहते हुए भी भारत में बाल- विवाह हो रहे हैं, क्यों? कारण बताइए।
Explain the aims and objectives of the Child Marriage Restraint Act 1929. Notwithstanding the Child Marriage Restraint Act, 1929 in the operation, child marriage are still solemonized in India, why? Give the reasons.
उत्तर- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निर्धन, अशिक्षित एवं निरक्षर है, जिसके कारण वे विभिन्न कुरीतियों से ग्रस्त हैं। इन सामाजिक कुरीतियों में एक ‘बाल विवाह’ है। भारत में यह परम्परा अतीत से चली आ रही है। प्रतिवर्ष यहाँ असंख्य अवयस्क व्यक्ति विवाह सूत्र में बंधते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी मुहूर्त के असंख्य बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। यहाँ तक की दूधमुँहे बच्चों के ब्याह भी रचा दिये जाते हैं। ऐसे करके बच्चों के अभिभावक अपने आपको बड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं। वे इसे अपने दायित्व की इतिश्री मान लेते हैं। लेकिन उन्हें ऐसे बाल विवाहों के भावी दुष्परिणामों का बोध नहीं होता।
वैसे इन बाल विवाह का प्रमुख कारण ‘अशिक्षा एवं अंधविश्वास’ है। क्योंकि एक अशिक्षित एवं अंधविश्वासी अभिभावक यह चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वह अपने बच्चों का विवाह सम्पन्न करा दे ताकि कोई अनिष्ट न हो। दूसरा कारण ‘निर्धनता’ है यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक लड़कियाँ हैं तो निर्धनता के कारण वह वयस्क अवयस्क सभी का एक साथ विवाह कराने को विवश हो जाता है ताकि अधिक व्यय न हो। तीसरा कारण ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ का प्रश्न है। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि अधिक आयु में बच्चियों या बच्चों का विवाह करने से सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है।
इन सामाजिक कुरीति का निवारण करने के लिए सन् 1929 में ‘बाल विवाह अवरोध अधिनियम’ पारित किया गया। समय-समय पर इसमें संशोधन भी किये गये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन सन् 1978 में किये गये। इस अधिनियम की धारा 2 में बालक से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिसने, यदि पुरुष है तो, 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
बाल विवाह अवरोध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम हो बाल विवाह करता है, तो उसको हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में दिये गये साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जयेगा। यानि कि उसे हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत 15 दिन तक के साधारण कारावास या रुपया 1000/- तक के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जायेगा। किन्तु वर्तमान में 2007 के संशोधन के बाद अधिनियम में यह प्रावधान दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 5 के खण्ड (3) में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करेगा तो (जिसमें शर्त यह है कि विवाह के समय वर 21 वर्ष का हो तथा कन्या 18 वर्ष को हो) तो ऐसी शर्तों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास से अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
यदि कोई पुरुष, जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, 15 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 3 वर्ष तक के साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 की धारा 5 के अनुसार जो बाल विवाह रचायेगा उसे भी समान दण्ड से दण्डित किया जायेगा जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि उसे यह विश्वास था कि विवाह बाल विवाह नहीं था। धारा 6 के अनुसार यदि कोई अवयस्क बाल विवाह करता है, तो जिसके नियन्त्रण में रहते हुए वह अवयस्क विवाह करता है उसे 3 माह तक के साधारण कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। लेकिन स्त्री को दण्डित नहीं किया जायेगा। जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये, यही माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने बाल विवाह रोकने में असावधानी बरती है, जिसके नियन्त्रण में रहते हुए अवयस्क ने बाल विवाह किया है।
स्पष्ट है कि बाल विवाह के लिए माता-पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे विवाह का निश्चय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो।
बाल विवाह के लिए उत्प्रेरित करना अथवा उकसाना भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह के लिए पुरोहित को भी दण्डित किया जा सकता है, यदि वह जान-बूझकर बाल-विवाह सम्पन्न कराता है। लेकिन बाल-विवाह में सम्मिलित होना मात्र दण्डनीय नहीं है। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यदि बाल विवाह हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है तो ऐसे मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।
इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि एवं दण्डित करने के लिए यह तथ्य सन्देह से परे साबित हो जाना चाहिए कि तथाकथित विवाह बाल विवाह ही था।
कान्तिलाल बनाम प्रेमचन्द्र, (1990) क्रि० लॉ ज० 456 राजस्थान के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि लड़के एवं लड़की की आयु के सम्बन्ध में न तो किसी को जानकारी हो और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।
बाल विवाह के लिए ऋण
परशुराम बनाम श्रीमती नारायणी देवी, ए० आई० आर० (1972) इलाहाबाद 357, के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी अवयस्क व्यक्ति के विवाह के लिए अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा ऋण लिया जाता है, तो उसे विधिक आवश्यकता के लिया गया ऋण माना जायेगा और वह वसूली योग्य होगा।
बाल विवाह शून्य नहीं होता – बाल विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अवश्य है लेकिन वह न तो शून्य है और न ही अविधिमान्य। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति मात्र इस आधार पर बाल-विवाह से उद्भूत अन्य दायित्वों से बच नहीं सकता है कि ऐसा विवाह बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है।
प्रक्रिया – बाल विवाह अवरोध अधिनियम की परिधि में आने वाले अवरोधों को कतिपय प्रयोजनों के लिए संज्ञेय माना गया है। ऐसे मामलों का विचारण केरने की ‘अधिकारिता’ महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। अधिकारिता का विनिश्चित विवाह स्थल के आधार पर किया जाता है, तिलक के स्थान पर नहीं।
प्रसंज्ञान लेने की अवधि अपराध कारित किये जाने की तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी है। अपराधों की जाँच एवं विचारण परिवाद पेश किये जाने पर किया जाता है। किसी भी परिवाद को बिना जाँच के खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक आज्ञापक व्यवस्था है।
बाल विवाह रोकने के लिए व्यादेश- अधिनियम की धारा 12 अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए व्यादेश जारी किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। जब भी न्यायालय को परिवाद पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के उल्लंघन में-
(i) कोई बाल विवाह होने वाला है, या
(ii) किसी बाल विवाह का ठहराव हो गया है, या
(iii) उसका अनुष्ठान होने वाला है, तो न्यायालय ऐसे विवाह को रोकने के आंशय का आदेश जारी कर सकेगा।
लेकिन ऐसा व्यादेश जारी करने से पूर्व विपक्षी को हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यादेश का शासय उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह तक की अवधि के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसे दण्डित करने से पूर्व उसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे व्यादेश की जानकारी थी या नहीं। धारा 12 के अन्तर्गत व्यादेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य बाल विवाहों का सम्पन्न होने से पहले ही रोक देना है।
इस प्रकार बाल विवाह अवरोध अधिनियम बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के निवारण की दशा में एक उत्कृष्ट कदम है, परन्तु इस अधिनियम में कई खामियाँ हैं जैसे इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत कम सजा का प्रावधान है तथा यह कानून भी काफी लचीला है, जिसकी वजह से बाल विवाह रोकने हेतु प्रावधान होते हुए भी भारत के अनेक राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा बिहार जैसे राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं।
प्रश्न 16. ‘सती’ शब्द को परिभाषित कीजिए। सती (निवारण) अधिनियम के पारित होने के उद्देश्यों को बतलाइये।
उत्तर- सती से अभिप्राय – सती (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार सती होने से अभिप्राय है- (i) “मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना।” या
(ii) किसी स्त्री की उसके किसी सम्बन्धी के शव के साथ, इस तथ्य को बिना विचार किये कि, ऐसा गाड़ना या जलाना, उस विधवा या स्त्री द्वारा उसकी ओर से स्वैच्छिक या अन्यथा।
वस्तुतः सती में होता भी यही है। मृतक पति की विधवा अपने पति के शव के साथ चिता में बैठकर अपना प्राण त्यागती है।
वैसे किसी स्त्री को सती अथवा पवित्र कहना न तो बुरा है और न ही अपराध। अपराध है विधवा का जलकर मरना।
सती को गौरवान्वित करने से तात्पर्य धारा 2 (1) (ब) के अनुसार-
(i) सती के सम्बन्ध में कोई जुलूस निकालना या उत्सव मनाना, अथवा
(ii) सती प्रथा को किसी भी प्रकार न्यायोचित ठहराना, समर्थन करना या प्रचार करना, अथवा
(iii) जिसने सती की ही हो उस व्यक्ति की स्तुति करने के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन करना, अथवा
(iv) किसी व्यक्ति के जिसने सती किया हो कि स्मृति सुरक्षित रखने या उसके सम्मान को स्थायी बनाने के विचार से किसी न्यास का निर्माण करनी, या राशि का एकत्रित करना, अथवा किसी मन्दिर का निर्माण; या कोई ऐसा निर्माण, जिसमें किसी उत्सव या किसी भी रूप में उसकी आराधना की जा सके, भी शामिल है।
इस अधिनियम के अन्तर्गत सती विषयक निम्नलिखित कार्यों का निषेध किया गया है जो इस प्रकार है-
(क) सती होने का प्रयास करना,
(ख) सती होने के लिए दुष्प्रेरित करना, तथ
(ग) सती को गौरवान्वित करना।
किसी को अपने मृतक पति के शव के साथ जलने या दफन होने के लिए उत्प्रेरित करना दुष्प्रेरण है। इसमें निम्नांकित कार्य सम्मिलित हैं-
(1) सती होने के लिए उकसाना,
(2) सती से आत्मिक लाभ होने जैसा बातें करना,
(3) किसी महिला के सती होने के निर्णय में भाग लेना,
(4) सती के साथ कब्रिस्तान तक जुलूस में जाना, नारे लगाना,
(5) सती स्थल पर उपस्थित रहना तथा सती होने कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाना
(6) सती होने से रोकने वाली कार्यवाही में बाधा या विघ्न उत्पन्न करना आदि।
दुष्प्रेरण के अपराध के गठन के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अपराध को कारित करने में अपराधी द्वारा सहायता की गयी थी। थोराम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, (1985) 3 एस० सी० सी० 495, में इस अधिनियम की परिधि में आने वाले निम्नांकित कार्यों को अपराध मानते हुए उनके लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी है-
(1) सती होने का प्रयास करने पर मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माना।
(2) सती को गौरवान्वित किये जाने पर न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम सात वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा न्यूनतम पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना।
ओंकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, (1987) 2 आर० एल० आर० 957, के मामले में यह कहा गया है कि सती प्रथा के निवारण हेतु बाहरी प्रतिबन्धों को जिस प्रकार उचित माना जाता है उसी प्रकार के प्रतिबन्ध सती स्थल और मन्दिरों पर भी लागू किये जाने चाहिए। सती-स्थलों एवं मन्दिरों को संरक्षण प्रदान किया जाना उचित नहीं है।
निवारक कार्य – अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 में कलेक्टर को सती विषयक कृत्यों को रोकने की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। इन शक्तियों के अन्तर्गत कलेक्टर-
(1) आदेश जारी कर सती होने वाली स्त्री के लिए दुष्प्रेरणाजन्य कार्यों पर रोक लगा सकता है,
(2) सती को गौरवान्वित किये जाने वाले कार्यों, उत्सवों, समारोहों, जुलूसों आदि पर रोक लगा सकता हैं,
(3) सती-स्थल, मन्दिर निर्माण आदि को ध्वस्त किये जाने का आदेश दे सकता है, तथा
(4) सती विषयक क्रिया-कलापों के लिए एकत्रित निधि को समपहत कर सकता है। कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना किये जाने पर दोषी व्यक्ति को न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम सात वर्ष तक की अवधि के कारावास तथा न्यूनतम 5,000 रुपये तथा अधिकतम 30,000 रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
सद्भावनापूर्वक कार्यों के लिए संरक्षण – अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के लिए वाद् अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है।
यहाँ “शब्द” सद्भावनापूर्वक महत्वपूर्ण है। संरक्षण का लाभ केवल तभी मिल सकता है जब ऐसा कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाय। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बेरिक, ए० आई० आर० (1987) एस० सी० 1265 ।
इस अधिनियम में दो बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है-.
(1) विधवा सामाजिक माहौल और दबाव से पीड़ित है न कि वह अपराधी है।
(2) सती का उत्सव मनाने या गौरव बढ़ाने के लिए चन्दा प्रायः व्यक्ति विशेष द्वारा न देकर बल्कि निगमित इकाइयों द्वारा प्रचार हेतु टैक्स बचाने के लिए दिया जाता है।
इस अधिनियम के बनने के पूर्व सती जैसे मामलों में अभियुक्तों को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत उत्तरदायी ठहराया जाता था। निनाद डी० सेठ के अनुसार सती अधिनियम बनाने के बजाय सरकार को सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोग ऐसे कार्य से घृणा करें। उनके कथनानुसार सती प्रथा की बुरायो को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि इसके पीछे मनोभावना को समझा जाये। राज्य ने सामाजिक परिवर्तन की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के बजाय कानून बनाने का आसान रास्ता चुन लिया। वास्तव में समाज को विधवा स्त्रियों के प्रति भवनाओं को बदलना चाहिए। आज भी अधिकतर विधवा स्त्रियाँ पान खाना सुगन्धित वस्तुओं, पुष्प, जेवरात, रंगीन वस्त्रों का प्रयोग दिन में दो बार भोजन करना आँखों में काजल लगाना आदि छोड़ देती हैं। वे सफेद कपड़े पहनती हैं गुस्सा जब्त करती हैं और जमीन पर सोती हैं।
हारवर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट ने मार्टी चेन लन्दन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स के जीन ड्रेस द्वारा संयुक्त रूप से अप्रैल, 1994 में बंगलौर में आयोजित विधवाओं के सम्मेलन में विधवा महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता नजर आयी। सम्मेलन में विधवाओं को मुख्य माँग यह थी कि मायके में या ससुराल में उनका मकान होना चाहिए। भूमि, जल आदि उत्पादक स्रोतों, मुख्य रूप से कृषि से सम्बन्धित उपकरणों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सम्मेलन में भाग लेने वाली कई महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें आश्रय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाय तो वे बिना आदमी के भी रह सकती हैं।
अब हम इक्कीसवीं शताब्दी में पहुँच चुके हैं। यदि हम भविष्य में निर्दोष महिलाओं की जिन्दगी बचाना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में और अधिक जागरुकता की आवश्यकता है।
आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में देवदासी प्रथा काफी प्रचलित है। उड़ीसा में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा काफी विरोध करने के बावजूद राज्य द्वारा इस प्रथा को जीवित रखने हेतु संघर्ष किया जा रहा है। इस परम्परा में लड़कियाँ बहुत हो अल्प आयु में मंदिरों में धर्मार्थ समर्पित कर दी जाती हैं। वह पुरोहित के नियन्त्रण में रहती हैं और कहा जाता है कि धर्म के नाम पर पुरोहित तथा अन्य लोग उनका यौन शोषण करते हैं। वर्तमान शताब्दी में भी इस सामाजिक बुरायी द्वारा कई लड़कियों का जीवन बर्बाद किया जा चुका है। यह छोटी बच्चियों के यौन शोषण का सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं की निष्क्रीयता द्वारा क्षमादान है जो कि महिलाओं का स्तर ऊँचा उठाने की डोंगें मारते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में केवल इतना कहा कि देवदासियाँ इस प्रथा के सम्बन्ध में सरकार के रवैये के विरुद्ध विद्रोह कर रही हैं। गौरव जैन बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1997) एस० सी० 3021, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को वेश्यावृत्ति रोकने तथा उनकी सन्तानों के पुनर्वास के लिए समुचित कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे कलंकित पेशे में महिलाओं को रोकने का समुचित उपाय करें तथा जो ऐसे पेशे में चली गई हैं उनकी सन्तानों को ऐसे पेशे को अपनाने से रोकने के लिए प्रयास करें तथा उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करें जिससे वे मानव गरिमा का जीवन जी सकें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का लक्ष्य है। आर्थिक पुनर्वास ऐसी महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह भी आवश्यक है कि इन लेगों को पुनर्सामाजीकरण कार्यक्रमों में लगाया जाये जो इन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करे तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से इलाज करें। यह रूढ़िवादी समाज की अमानवीयता का प्रमाण है कि 16,000 से अधिक बंगाली विधवा महिलाओं को मथुरा, वृन्दावन और वाराणसी के हिन्दू तीर्थ स्थानों दरिद्रता का जीवन बिताने के लिए भेज दिया गया। बात यह है कि इस प्रकार का निर्वासन जो अंग्रेजों के शासन काल में प्रारम्भ हुआ था, आज भी विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बहुत सी नवयुवतियों तथा वृद्ध महिलाओं को उनके पैतृक घर से कई कारणों से निकाल दिया जाता है। यह कारण सदैव ईश्वर के दर्शन करने के लिए नहीं होते हैं। पति की मृत्यु के उपरान्त, विधवा महिलायें, अन्य पुरुषों द्वारा उनकी सम्पत्ति हड़पने के लिए घर से निकाल दी जाती है। इस तरह का कार्य यहाँ तक कि पुत्रों एवं दामाद द्वारा भी किया जाता है।
हिन्दू स्त्रियों के उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानून होते हुए भी, वे इससे वंचित रहती हैं क्यूँकि उन्हें अपने अधिकारों से सम्बन्धित कानून की जानकारी नहीं होती है या फिर वे अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के दबाव के कारण आवाज उठाने में असमर्थ होती हैं। यदि घर से नहीं भी निकाला जाता है तो प्रायः उन्हें एकान्त जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाता है और परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा उनका यौन शोषण होता है। वास्तव में जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है, पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है ‘तथा उन्हें और अधिक सम्मान के साथ घर पर रखना चाहिए। साथ ही सरकार तथा महिला संगठनों को चाहिए कि वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें। तभी विधवा स्त्रियों का निर्वासन और उनके विरुद्ध अन्य क्रूरताएँ समाप्त हो सकती हैं।
प्रश्न 17. सती होने के लिए दुष्प्रेरित करना एवं सती विषयक अन्य निषेधित कार्यों का वर्णन करते हुए इन अपराधों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों या जिलाधीश की शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर- वर्तमान सती विरोधी अधिनियम उन तमाम कानूनों के स्थान पर जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थे, केन्द्रीय कानून के रूप में रखा गया है। यह अधिनियम सती हेतु न केवल निषेध और दण्ड की व्यवस्था करता है बल्कि सती की प्रशंसा करने को भी अपराध की श्रेणी में लाता है।
वित्तीय या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के आपराधिक शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अधिनियम में उपबन्ध किये गये हैं। अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सती होता है, तब जो कोई ऐसे सती होने का प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण करता है, वह मृत्युदण्ड से या कारावास से दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
सती (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 4 (2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सती होने का प्रयास करता है तब जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रयास का दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
इस धारा के प्रयोजन के लिए, निम्न में से कोई एक कार्य को या उसी के समान कृत्य को दुष्प्रेरण माना जायेगा –
(क) किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ अथवा किसी अन्य रिश्तेदार से सम्बन्धित हो, के साथ जीवित जलाने या गाड़े जाने के लिए फुसलाना, चाहे वह मानसिक रूप से उचित दशा में हो अथवा किसी प्रकार की मूर्छा या उन्मत्त होने से या अन्य किसी कारण से अपनी स्वतन्त्र इच्छा का प्रयोग करने में असमर्थ हो;
(ख) किसी विधवा या स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती होने से उसके मृत पति या उसके रिश्तेदार या उसके परिवार की सामान्य अच्छाई होगी या उनको आत्मिक लाभ होगा।
(ग) किसी विधवा या किसी स्त्री को सती होने के निर्णय पर दृढ़ रहने के और इस प्रकार सती होने के लिए उकसाना;
(घ) सती होने के किसी विधवा या स्त्री के निर्णय में सहायता करना, उसे उसके मृत पति के शव के साथ या उसके रिश्तेदार के शव के साथ श्मशान या कब्ररिस्तान में ले जाना अथवा सती होने से सम्बन्धित किसी जुलूस में भाग लेना;
(ङ) किसी ऐसे स्थान में जहाँ सती हो रही हो सक्रिय रूप से उपस्थित रहना, भाग लेना या उससे सम्बन्धित किसी उत्सव में उपस्थित रहना या भाग लेना;
(च) किसी स्त्री या विधवा द्वारा जीवित जलाये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में किये जाने वाले कर्तव्यों में बाधा डालना या अवरोध करना।
सती का गौरव बढ़ाने के लिए शास्ति [ धारा 5]- जो कोई सती का गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष को हो सकेगी किन्तु जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये से कम का नहीं हेगा, किन्तु जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।
सती अपराध के रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधिकार- सती (निवारण) अधिनियम की धारा 6 के अनुसार-
(i) जहाँ कलेक्टर या जिला दण्डाधिकारी का यह विचार है कि, सती या उसका दुष्प्रेरण हो रहा है या होने वाला है तो वह आदेश द्वारा, सती से सम्बन्धित किसी ऐसे कार्य को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र में या आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्रों में, किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
(ii) कलेक्टर अपने आदेश द्वारा किसी प्रकार से सती को, गौरवान्वित करने के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र में या आदेश से निर्दिष्ट क्षेत्रों में, आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगा सकता है।
(iii) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश का उल्लंघन ( करता है और यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन के दण्ड का उपबन्ध नहीं है वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा लेकिन जो पाँच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, से भी दण्डनीय होगा।
किसी मन्दिर या निर्माण को हटाने का अधिकार- अधिनियम की धारा 7 के अनुसार-
(i) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई मन्दिर या निर्माण, जो बीस वर्ष से कम न होने वाली अवधि से अस्तित्व में है, से किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसके द्वारा सती किया गया है, किसी भी प्रकार की आराधना, या
उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आशय उसकी याद को सुरक्षित रखना या उसके प्रति सम्मान को बढ़ाना है, आदेश द्वारा ऐसे मन्दिर या निर्माण को हटाये जाने का निर्देश दे सकती है।
(ii) यदि जिला दण्डाधिकारी या कलेक्टर को यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी मन्दिर या अन्य निर्माण के सिवाय, किसी मन्दिर या निर्माण में किसी व्यक्ति जो सती हुयी है, के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना या उत्सव इस आशय से, कि उसकी याद को सुरक्षित रखा जाये या सम्मान को बढ़ाया जाये, या किया जा रहा है तो वह आदेश द्वारा ऐसे मन्दिर या निर्माण को हटाये जाने का निर्देश दे सकता है।
(iii) जहाँ उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी आदेश का पालन नहीं किया जाये, तो राज्य सरकार या कलेक्टर या जिला दण्डाधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसका पद उपनिरीक्षक से कम न होगा, ऐसे मन्दिर या निर्माण को, दोषी पाये जाने पर, हटाया या तुड़वा सकेगा।
सम्पत्तियों को समपहृत करने की शक्ति- सती (निवारण) अधिनियम की धारा 8 के अनुसार-
(i) जहाँ कलेक्टर को यह विश्वास करना उचित कारण है कि कोई निधि एकत्रित की गयी है या सम्पत्ति अर्जित की गयी है, जिसका आशय सती होने को गौरवान्वित करना है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पायी जाती है कि जिससे यह सन्देह हो कि इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित होगा, तो वह ऐसी निधि या सम्पत्ति को समपहृत (जब्त) कर सकता है।
(ii) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलेक्टर या जिला दण्डाधिकारी इस अधिनियम के अधीन गठित सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय को, यदि कोई हो, ऐसी निधि या सम्पत्ति के समपहरण की सूचना देगा या और ऐसी सम्पत्ति के निराकरण के लिये विशेष न्यायालय के आदेश की प्रतिरक्षा करेगा।
अध्याय 6
लज्जा भंग एवं बलात्कार
(Outrage of Modesty and Rape)
प्रश्न 18. महिलाओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित अपराधों की व्याख्या कीजिए-
(क) लज्जा भंग
(ख) बलात्कार
(ग) अप्राकृतिक अपराध
(घ) लज्जा का अनादर
From the Point of view of Women explain the following offences:
(a) Outrage of Modesty
(b) Rape
(c) Unnatural offence
(d) Insult of Modesty
उत्तर (क) – लजा भंग (Outrage of Modesty) – लज्जा महिला का आभूषण होता है। प्रत्येक महिला अपनी लज्जा अथवा शील की रक्षा करना चाहती है, चाहे यह किसी भी आयु की क्यों न हो। स्त्री की परिभाषा में ही उसकी लज्जा को सम्मिलित किया गया है। स्त्री चाहे बालिका हो या प्रौढ़, उसमें शील अथवा लज्जा निहित रहती है। यही कारण है कि लज्जा भंग को विधि के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध माना गया है।
लज्जा नारी का एक सहज स्वभाव होता है। स्त्री चाहे वह किसी भी उम्र की क्यों न हो उसमें लज्जा होती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 10 में स्त्री की परिभाषा दी गयी है। इसके अनुसार “स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।” यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा अथवा उसके शील को भंग करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है “जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।”
पंजाब राज्य बनाम मेजन सिंह, ए० आई० आर० (1967) एस० सी० 63, के वाद में अभियुक्त द्वारा एक साढ़े सात माह की बालिका की योनि में उंगली डालकर उस पर अश्लील हमला किया। वह नंगा होकर बच्ची पर लेट गया। अभियुक्त की ओर से बचाव में यह तर्क दिया गया कि धारा 354 के अपराध के लिए स्त्री की लज्जा भंग होना आवश्यक है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए अभियुक्त को धारा 354 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया। न्यायाधीश महोदय का अभिकथन था कि महिला स्त्री की आयु कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह बुद्धिमान हो या मन्द बुद्धि, जाग रही हो या सो रही हो, उसकी लज्जा सदैव उसके ‘स्त्री देह’ के साथ रहती है और जिसे भंग किया जा सकता है।
पांडुरंग सीताराम भागवत बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए० आई० आर० (2005) एस० सी० 643, के बाद में परिवादिनी ने अभिकथित किया कि जब उसका पति बाहर गया हुआ था, तब अभियुक्त उसके कमरे में प्रवेश किया और उसे पीछे से आलिंगन करते हुए उसके वक्षस्थल का स्पर्श कर उसकी लज्जा भंग की। लज्जा भंग के मामले में यह सिद्धान्त कि ‘सामान्यतः’ कोई भी महिला अपने चरित्र को दाँव पर नहीं रखेगी सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर विनिश्चित किया जाना होता है। अतः अपीलार्थी को सन्देह का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया।
श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम के० पी० एस० गिल, ए० आई० आर० (1996) एस० सी० 309 के एक मामले में जहाँ श्रीमती बजाज एक आई० ए० एस० अधिकारी थीं। घटना के समय वह पंजाब सरकार के वित्त विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं। दिनांक 18 जुलाई, 1988 का वह एस० एल० कपूर के यहाँ दावत में गयी थीं। उस दावत में पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। दावत में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के० पी० एस० गिल भी आमन्त्रित किये गये थे। देवल का कहना था कि रात्रि के करीब 10 बजे के० पी० एस० गिल उसके पास आये और उसके कूल्हे पर मारी। देवल को यह बहुत बुरा लगा और उसके द्वारा गिल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 342, 352, 354 एवं 509 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया। के० पी० एस० गिल ने इसे न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने इसे संहिता की धारा 354 एवं 509 के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला माना और विचारण के निर्देश दिये। अन्ततः विचारण में भी गिल को धारा 354 के अन्तर्गत अपराध का दोषी माना गया।
उल्लेखनीय है कि लज्जा भंग के कृत्य देश की संस्कृति पर निर्भर करते हैं। स्त्री का चुम्बन लेना, उसके हाथ को चूमना, कूल्हा थपथपाना आदि किसी देश की संस्कृति के अंग हो सकते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति में इन कृत्यों को सामान्यतया हेय समझा जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ इन्हें अपराध माना गया।
प्रेमिया उर्फ प्रेमप्रकाश बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए० आई० आर० (2009) एस० सी० 351 के मामले में अभियोक्त्रि द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त ने अपना पायजामा खोला, अभियोक्त्री के घाघरे को ऊपर उठाया और उसके साथ बलात्कार किया। इसमें अभियोक्ती द्वारा लैंगिक सम्भोग के किसी विनिर्दिष्ट कार्य का उल्लेख नहीं किया गया। अभियुक्त को स्त्री की लज्जा भंग करने का दोषी माना गया, बलात्कार का नहीं।
उत्तर (ख) – बलात्कार (Rape)- बलात्संग या बलात्कार स्त्री के विरुद्ध किया जाने वाला गम्भीरतम अपराध है। बलात्संग की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में की गई है। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने इस धारा में उल्लिखित पाँच परिस्थितयों में से किसी एक परिस्थिति के अन्तर्गत किसी स्त्री के साथ बलात् सम्भोग किया है तो यह कहा जायेगा कि उसने उस स्त्री के साथ बलात्संग किया है तथा वह बलात्संग के अपराध के लिए दण्डित किया जायेगा। साधारण अर्थ में, किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसके साथ जबरन सम्भोग करना ही बलात्संग या बलात्कार है। सम्मति का अर्थ स्वतन्त्र सहमति है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ सम्भोग करने के लिए उससे जबरन या भय दिखाकर सम्मति प्राप्त करता है तो भी वह बलात्संग के अपराध का दोषी है। बलात्संग (Rape) के अपराध के निम्न आवश्यक तत्व हैं-
(1) बलात्संग के अपराध का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि यह किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष द्वारा उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया सम्भोग है। यहाँ पुरुष की परिभाषा, जैसा कि धारा 10 में की गई है, किसी भी आयु के नर को पुरुष मानती है। सात वर्ष से बारह वर्ष के बालक इस परिभाषा से उन्मुक्त हैं। इस प्रकार पुरुष वह नर है जो बारह वर्ष से अधिक आयु-प्राप्त है।
(2) बलात्संग के अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित (धारा 375 में उल्लिखित) परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में सम्भोग किया हो। ये परिस्थितियाँ निम्न हैं-
(क) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध– स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अर्थात् स्त्री की सहमति के विरुद्ध। यहाँ यह आवश्यक है कि स्त्री ने यह जानते हुए कि उसके साथ क्या किया जाना है, अपनी सहमति दी हो। स्त्री को आपत्ति व्यक्त करने का ज्ञान हो या स्त्री अपनी सहमति व्यक्त करने में सक्षम हो। यह स्मरणीय है कि इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना दोनों एक नहीं हैं। उदाहरणार्थ-यदि कोई पुरुष किसी सोयी हुई या मत्त या बेहोश स्त्री के साथ सम्भोग करता है तो वह जागने पर या होश में आने पर सहमति दे सकती है, परन्तु उसके साथ किया गया सम्भोग उसकी इच्छा के विरुद्ध माना जायेगा। इस प्रकार ‘इच्छा के विरुद्ध’ शब्दावली सम्मति के विरुद्ध शब्दावली से अधिक विस्तृत है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री जादू-टोने या तथ्य की भूल के कारण सम्भोग हेतु सहमत हो जाती है तो यह नहीं कहा जाता कि सम्भोग के लिए उसकी इच्छा थी।
(ख) सहमति के बिना – किसी भी स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ किया गया सम्भोग बलात्संग का अपराध माना जायेगा। सहमति सम्भोग कार्य से पूर्व होनी चाहिए। सम्भोग के पश्चात् दी गई सहमति का कोई महत्व नहीं है।
आर० बनाम विलियम, (1923) के० बी० 340 नामक वाद में अभियुक्त एक संगीत-शिक्षक था। उसने अपनी शिष्या के साथ यह कहकर सम्भोग किया कि इस कार्य से उसका सुर मधुर हो जायेगा। इस सहमति को कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त सहमति मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को बलात्संग के अपराध का दोषी माना।
एक व्यक्ति एक स्त्री से यह कहकर सम्भोग के लिए सहमति प्राप्त करता है कि सम्भोग के पश्चात् वह उससे विवाह कर लेगा। यदि वह सम्भोग करने के पश्चात् विवाह करने से मुकर जाता है तो भी वह बलात्संग के अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सहमति धोखे से प्राप्त की गई नहीं मानी जायेगी।
किसी स्त्री की सम्भोग के लिए सहमति थी या नहीं इसे निर्धारित करने के लिए किसी कठोर नियम को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्णीत किया जायेगा।
इस बिन्दु पर महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रकाश, ए० आई० आर० 1992 एस० सी० 1275 का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले में एक स्त्री को उसके पति के साथ गणेशोत्सव में एक सिपाही के माध्यम से बुलाया गया। उसके पति को गणेश जी की मूर्ति को अपवित्र करने का आरोप लगाकर मारा-पीटा गया तथा उसके पश्चात् महिला को कुछ हस्ताक्षर करने को कहा गया तथा ऐसा करने से इन्कार करने या महिला के पति को पुलिस हिरासत में भेजकर भवन- स्वामी तथा सिपाही ने एक के बाद उस महिला के साथ बलात्संग किया तथा उसके पति को शिकायत न करने के लिए धमकाया गया। दूसरे दिन उसके पति ने दोनों बलात्कारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की।
विचारण-न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। अपील में बम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अभियुक्तों को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि महिला के शरीर पर प्रतिरोध के कोई चिन्ह नहीं पाये गये। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को त्रुटिपूर्ण माना तथा यह निर्णय दिया कि बलात्संग के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित स्त्री के विरुद्ध बल-प्रयोग किया गया हो। बल प्रयोग की धमकी मात्र पर्याप्त है। वर्दीधारी सिपाही से भयभीत होना तथा उसके कहने पर अभियुक्त के यहाँ जाना महिला की विवशता थी। अभियुक्त यह साबित नहीं कर पाये कि महिला तथा उसका पति उन्हें क्यों तथा किस दुराशय से फँसायेंगे।
(ग) मृत्यु या चोट का भय दिखाकर प्राप्त की गयी सम्मति– यदि कोई स्त्री मृत्यु या चोट के भयवश अपने शरीर के समर्पण के लिए सहमत हो जाये तो उसे स्वतन्त्र सहमति नहीं कहा जा सकता। यह भय या तो स्वयं या उसके हितबद्ध के शरीर को क्षति करने के सम्बन्ध में हो सकता है।
(घ) धोखे से प्राप्त की गई सहमति- यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अपने को उसका पति बताकर सम्भोग हेतु सहमति प्राप्त करता है या कोई ऐसा कथन कर सहमति प्राप्त करता है जो सत्य नहीं है तो ऐसी सहमति स्वतन्त्र नहीं मानी जायेगी। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि सम्भोग से स्वर मधुर हो जायेगा या सम्भोग से लड़का होगा या सम्भोग से स्वर्ग या आध्यात्मिक सुख मिलेगा तो यह धोखे से प्राप्त सहमति होगी।
(ङ) विकृतचित्तता या मत्तता या जड़ता के अधीन प्राप्त सहमति – यदि कोई स्त्री मत्तता, पागलपन या जड़ता के कारण इस कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ है तो उसके द्वारा की गई सहमति स्वतन्त्र नहीं मानी जायेगी।
(च) सोलह वर्ष से कम आयु की लड़की से प्राप्त सम्मति– इस नियम का एक अपवाद यह है कि यदि पति अपनी सोलह वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसका कृत्य बलात्संग नहीं माना जायेगा परन्तु ऐस ऐसी पत्नी की आयु पन्द्रह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु की पुष्टि जन्म-रजिस्टर के आधार पर की जायेगी।
यशवंत राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० 1992 एस० सी० 1683 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि बलात्कार की शिकार लड़की की आयु पन्द्रह वर्ष से कम है (अवयस्क है) तो उसके साथ सम्भोग बलात्कार माना जायेगा, चाहे इसके लिए बालिका की सहमति हो या न हो।
प्रवेशन (Penetration) – पृथ्वीचन्द बनाम हिमाचल प्रदेश, ए० आई० आर० 1989 एस० सी० 702 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के प्रत्येक मामले में यह आवश्यक नहीं है कि लिंग-प्रवेशन के कारण छिद्र विकीर्ण या वीर्यस्त्राव हुआ हो। यदि लिंग-प्रवेशन नहीं हुआ है तो बलात्कार का अपराध गठित नहीं होता। यह बलात्कार का प्रयास मात्र माना जाता है। यदि आंशिक प्रवेश के कारण योनिछिद्र को क्षति नहीं पहुँची तो भी धारा 375 के अन्तर्गत यह बलात्संग के अपराध के लिए पर्याप्त प्रवेशन माना जायेगा।
प्रिया पटेल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ए० आई० आर० (2006) एस० सी० 2639 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में महिला को सहयुक्त माना जाकर उसे अभियोजित नहीं किया जा सकता है।
उत्तर (ग)- अप्राकृतिक अपराध (Unnatural offence)- विकृत मानसिकता के कारण आजकल मनुष्य में अप्राकृतिक मैथुन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रकृति के विरुद्ध यौन-क्रीड़ायें करने में व्यक्ति आनन्द की अनुभूति करता है। कई बार स्त्री के विरोध पर भी वह प्रकृति विरुद्ध यौन क्रीड़ा करने से नहीं चूकता। यही कारण है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 में इसे अपराध घोषित किया गया है। धारा 377 का मूल पाठ इस प्रकार है-
जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव-जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इन्द्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
स्पष्टीकरण- इस धारा में वर्णित अपराध के लिये आवश्यक इन्द्रिय-भोग गठित करने के लिये प्रवेशन पर्याप्त है।
इस धारा के पाठ से स्पष्ट है कि निम्नांकित प्रकार के इन्द्रिय-भोग को अप्राकृतिक मैथुन माना गया है –
(i) पुरुष का पुरुष के साथ अर्थात् गुदा मैथुन;
(ii) पशु अथवा जीव-जन्तु के साथ; एवं
(iii) पुरुष की भाँति स्त्री के साथ अर्थात् गुदा मैथुन, मुख-मैथुन आदि।
इस प्रकार धारा 377 गुदा मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, वैकृत मैथुन, पशुगमन आदि को दण्डनीय अपराध घोषित करती है।
इस विषय पर ग्रेस जयमणि बनाम ई० पी० पीटर, ए० आई० आर० 1982 कर्नाटक 46 का एक महत्त्वपूर्ण मामला है। इसमें गुदा मैथुन के आधार पर पत्नी ने पति के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की याचिका पेश की थी। पत्नी का कहना था कि सम्भोग के समय पति अपना लिंग उसके (पत्नी के) मुँह में रखा करता था। साथ-साथ वह अपना लिंग उसके मलद्वार में भी रखा करता था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसे गुदा मैथुन मानते हुये विवाह- विच्छेद का एक अच्छा आधार बताया।
जमील बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए० आई० आर० (2007) एस० सी० 971 के मामले में अभियुक्त द्वारा एक छः वर्षीय बालिका के साथ गुदा मैथुन किया गया। इसे अप्राकृतिक अपराध माना गया।
इस प्रकार धारा 377 महिलाओं को अप्राकृतिक मैथुन से संरक्षण प्रदान करती है।
उत्तर (घ) – लज्जा का अनादर (Insult of Modesty) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 में प्रावधान है कि “जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।”
अतः यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके सामने अंग विक्षेप या अश्लील भावभंगिमा करता है, या उसे सुनाकर अश्लील शब्दों का उच्चारण करता है या उसके समक्ष अश्लील चित्र प्रदर्शित करता है, तो उसे इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा।
तारकदास गुप्ता बनाम सम्म्राद्, (1925) 28 बम्बई लॉ रि० 99, के वाद में अभियुक्त, जो कि एक स्नातक था, ने एक बंद लिफाफे में कुछ अश्लील बातें लिखकर किसी अंग्रेज नर्स को पोस्ट द्वारा भेजी जबकि अभियुक्त का नर्स से कोई परिचय नहीं था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के इस धारा के अन्तर्गत सिद्धदोष करते हुए विनिश्चय किया कि यद्यपि अश्लील सन्देश लिफाफे में बंद किया गया था, फिर भी वह उस नर्स के प्रति, जिसके नाम से लेटर भेजा गया था, अश्लील प्रदर्शन माना जाएगा जिससे उक्त नर्स की लज्जा का अनादर हुआ था।
बाँके बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आर० (1961) इला० 131, के बाद में अभियुक्त एक महिला के पास एकांत में गया तथा उसने उसके वस्त्रों को हटाकर अपने गुप्तांग का प्रदर्शन किया। अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध नहीं हो सका, फिर भी उसे धारा 509 के अधीन महिला की लज्जा के अनादर के अपराध का दोषी ठहराया गया।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 509 के प्रावधानों को अवशिष्ट उपबंधों (Residuary Provisions) के रूप में समाविष्ट किया गया है ताकि ऐसा कृत्य जो किसी भी अपराध की कोटि में न आता हो, परन्तु जिससे किसी स्त्री की लज्जा का अनादर होता हो, तो उसे इस धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जा सके।
अध्याय 7
अनैतिक व्यापार (Immoral Traffic)
प्रश्न 19. “अनैतिक व्यापार” क्या है? स्पष्ट करें।
What is Immoral Traffic? Explain.
उत्तर – अनैतिक व्यापार से अभिप्राय यहाँ मुख्य रूप से वेश्यावृत्ति से है। वेश्यावृत्ति आज की एक ज्वलन्त समस्या है। विश्व के प्रायः अधिकांश देशों में इसका प्रचलन है। यह बात अलग है कि कहीं यह वैधानिक है तो कहीं अवैधानिक। भारत में वेश्यावृत्ति को न केवल विधिक दृष्टि से अपितु नैतिक दृष्टि से भी एक घृणित कार्य माना गया है। इसका स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा व्यभिचार का है। यदि हम गहराई में जायें तो वेश्यावृत्ति के अनेक कारण मिलेंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह दुष्प्रवृत्ति केवल साधारण परिवारों में ही व्याप्त न होकर सम्पन्न परिवारों में भी इसका पूरा जोर है। भारतीय संस्कृति में इसे एक गम्भीरतम पाप माना गया है। यह सही है कि हमारे यहाँ देवदासी जैसी प्रथायें रही हैं लेकिन कालान्तर में वे भी मृत प्राय सी हो गईं।
जब से देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, तब से न केवल महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है अपितु उनके अनैतिक व्यापार की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। पाँच सितारा संस्कृति ने भी इस प्रवृत्ति में अभिवृद्धि की है। आज वेश्यावृत्ति चरम सीमा पर है। सम्पन्न वर्ग इसे विलासिता का साधन मानता है तो निर्धन वर्ग इसे अपनी विवशता बताता है। होटलों में, कोठों में और सड़कों के निकटवर्ती क्षेत्रों में यह धन्धा आज जोरों से चल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि शिक्षित एवं सम्पन्न व्यक्ति वेश्यावृत्ति को व्यवसाय मानकर इसे चला रहे हैं। इसी पर नियन्त्रण पाने के लिये संसद द्वारा सन् 1956 में “स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम” पारित किया गया। कालान्तर में सन् 1986 में इस अधिनियम का शीर्षक “अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956” कर दिया गया।
प्रश्न 20. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिये दण्ड की क्या व्यवस्था की गई है।
उत्तर – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 में वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध किये गये हैं इस धारा के अनुसार-
(1) कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबन्ध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबन्ध में काम करता है या सहायता करता है वह प्रथम दोषसिद्धि पर एक वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दो वर्ष से अन्यून और पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
(2) कोई व्यक्ति जो-
(क) किसी परिवार का किरायेदार, पट्टेदर अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुये ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के प्रयुक्त करने देगा; अथवा
(ख) किसी परिसर का स्वामी, पट्टाकर्ता या भू-स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भू-स्वामी का अभिकर्ता होते हुये उसके या उसके किसी भाग को यह जानते हुये पट्टे पर देता है कि उसका या उसके किसी भाग का वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जाना आशयित है अथवा ऐसे परिसर या उसके किसी भाग के वेश्यागृह के रूप में प्रयोग का जानबूझकर पक्षकार होगा;
प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा द्वितीय पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।
(2-क) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि उस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, यथास्थिति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में उपयोग किये जाने के लिये जानबूझकर अनुज्ञात कर रहा है, या उसे यह जानकारी है कि परिसर या उसके किसी भाग का वेश्यागृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यदि –
(क) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में परिचालन है जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है, इस आशय की रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन को गयी तलाशी के परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि परिसर या उसके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिये उपयोग किया जा रहा है; अथवा
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पायी गयी सभी वस्तुओं की सूची की एक प्रति ऐसे किसी व्यक्ति को दे दी जाती है।
(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के किसी परिसर या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष होने पर, कोई ऐसा पट्टा या करार, जिसके अधीन ऐसा परिसर पट्टे पर दिया गया है या उस अपराध के किये जाने के समय धारित है या अधिभोगाधीन है उक्त दोषसिद्धि की तारीख से शून्य और अप्रवर्तनशील हो जायेगा।
प्रश्न 21. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु कौन-कौन सी निवारक व्यवस्था की गई है? स्पष्ट करें।
उत्तर- वेश्यावृत्ति के निवारण हेतु निवारक व्यवस्था – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में वेश्यावृत्ति के निवारक हेतु निवारण व्यवस्था भी की गई है जो निम्न है-
(1) धारा 18 के अन्तर्गत वेश्यागृहों को बन्द करने तथा वेश्यागृहों से अपराधियों को बेदखल किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि किसी मजिस्ट्रेट को पुलिस से या अन्यथा इस आशय की रिपोर्ट मिलती है कि किसी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के भीतर किसी घर, कमरे, स्थान या उसके किसी भाग में वेश्यागृह चलाया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित जाँच के पश्चात् यह आदेश दिया जा सकेगा कि-
(क) सात दिन के भीतर ऐसे घर, कमरे अथवा स्थान के अधिभोगी को वहाँ से बेदखल कर दिया जाये, तथा
(ख) ऐसे आदेश पारित होने के पश्चात् सामान्यतः एक वर्ष के भीतर तथा यदि ऐसे घर, कमरे अथवा स्थान में कोई बालक या अवयस्क पाया जाये तो तीन वर्ष के भीतर मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पट्टे पर नहीं दिया जाये।
उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार यदि किसी अधिभोगी को इस अधिनियम की धारा 3 या 7 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तो ऐसे अधिभीगी को धारा 18 के अन्तर्गत बेदखल भी किया जा सकता है।
इस धारा के अधीन की जाने वाली जाँच संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसके लिये नियमित रूप से विचारण किया जाना आवश्यक नहीं है।
धारा 20 के अन्तर्गत वेश्याओं को किसी स्थान से हटाये जाने के बारे में उपबन्ध किया गया है। जब किसी मजिस्ट्रेट को इस आशय की इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी स्थान में कोई व्यक्ति वेश्या है तो वह उसे कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् –
(क) उसे उस स्थान से हट जाने का आदेश दे सकेगा, तथा
(ख) उसके उस स्थान में पुनः प्रवेश को निषिद्ध कर सकेगा।
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या देवी, ए० आई० आर० (1964) एस० सी० 416 के मामले में धारा 20 की वैधानिकता को चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 20 के उपबन्ध युक्तियुक्त होने से वैधानिक हैं। इसी मामले में यह भी तय किया गया है कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द “इत्तिला मिलने पर” से आशय किसी विशेष पुलिस अधिकारी की इत्तिला से नहीं है। ऐसी इत्तिला किसी को भी हो सकती है।
2. वेश्यावृत्ति में लिप्त व्यक्ति को संरक्षागृह में रखा जाना
धारा 19 में की गयी व्यवस्था के अनुसार कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कर रहा है या जिससे वेश्यावृत्ति करा रहा है या जिससे वेश्यावृत्ति करायी जा रही है, उस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगी कि उसे-
(क) किसी संरक्षागृह में रखा जाये, या
(ख) किसी सुधार संस्था में भेजा जाये, या
(ग) किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाये।
इस प्रकार “अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956” वेश्यावृत्ति के निवारण की दिशा में पारित एक पूर्ण विधायन है। यह अधिनियम न केवल वेश्यावृत्ति का निवारण करता है, अपितु वेश्याओं के सुधार की दिशा में समुचित प्रावधान करता है।
प्रश्न 22. कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न की समस्या की विवेचना कीजिए।
Discuss Problems of exploitation and sexual harassment of women in Workplace.
उत्तर- जब से नारी स्वातन्त्र्य की लहर चली है तभी से महिलायें कर्म क्षेत्र में आगे आयी हैं। आज कई सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में महिलायें कार्यरत हैं। उनकी सफलता से महिलाओं का इन क्षेत्रों में आने का आकर्षण भी बढ़ा है। लेकिन कुछ वर्षों से कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनायें बढ़ने से उनमें निराशा उत्पन्न हुयी हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए० आई० आर० (1997) एस० सी० 3011 का ऐसा ही एक मामला आया, जिसमें कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिये न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश जारी किये गये, यथा-
(i) जहाँ कामकाजी महिलायें हैं, वहाँ के नियोजकों एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें, उन्हें रोकने के उपाय करें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें।
(ii) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायें तथा उत्पीड़न के दुष्परिणामों से जनसाधारण को अवगत कराया जाये।
(iii) यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न के लिये अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़ित महिला एवं मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को तंग व परेशान न किया जाये।
(iv) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को जाये।
(v) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न परिवादों (शिकायतों) की सुनवाई के लिये शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाये।
(vi) ऐसे समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जाये।
(vii) यौन उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाये तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये।
(viii) किसी कामकाजी महिला के साथ बाहरी व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न किये जाने पर ऐसी महिला को संरक्षण प्रदान किया जाये।
(ix) केन्द्र एवं राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित कानून बनायें।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा शब्द “यौन उत्पीड़न” को परिभाषित भी किया गया है। यौन उत्पीड़न में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है-
(क) शारीरिक सम्पर्क करना अथवा ऐसे सम्पर्क का प्रयास करना;
(ख) यौन सम्पर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध करना;
(ग) अश्लील टिप्पणियाँ अथवा संकेत करना;
(घ) कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन करना;
(ङ) अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण करना।
कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मामला वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बनाम ए० के० चोपड़ा, ए० आई० आर० (1999) एस० सी० 625 का है।
ए० के० चोपड़ा कौन्सिल के अध्यक्ष का निजी सचिव था। उस पर यह आरोप था कि उसने दिनांक 12.8.1988 को कौन्सिल की एक महिला कर्मचारी की लज्जा भंग करने का प्रयास किया था। वह महिला कर्मचारी कौन्सिल में क्लर्क कम-टाईपिस्ट के पद पर कार्यरत थी लेकिन वह डिक्टेशन लेने में सक्षम नहीं थी। घटना के दिन ए० के० चोपड़ा ने उस महिला कर्मचारी को कौंसिल के अध्यक्ष से डिक्टेशन लेने और टाईप करने हेतु ताज पैलेस होटल के व्यापार केन्द्र में आने को कहा। वह महिला कर्मचारी ताज पैलेस होटल पहुँची और वहाँ पर वह एक कमरे में निदेशक की प्रतीक्षा करने लगी। ए० के० चोपड़ा भी वहाँ उपस्थित था। उसने निरन्तर उस महिला कर्मचारी से शारीरिक सम्पर्क करने का प्रयास किया। वह बार-बार उसके पास बैठने का प्रयास करता रहा। जब उस महिला कर्मचारी ने निदेशक से डिक्टेशन ले लिया तब ए० के० चोपड़ा ने उस ‘डिक्टेशन को टाईप करने के लिये महिला कर्मचारी को ताज पैलेज होटल के तलघर में जाने को कहा। वह महिला कर्मचारी तलघर में पहुँची जहाँ उसने डिक्टेशन को टाईप किया। इस दौरान भी ए० के० चोपड़ा ने उस महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हरकतें की। उल्लेखनीय है कि ए० के० चोपड़ा द्वारा उस महिला कर्मचारी के साथ लिफ्ट में भी आपत्तिजनक कृत्य किये जाने की चेष्टा की गयी थी लेकिन उस महिला कर्मचारी के प्रतिरोध करने के कारण वह सफल नहीं हो सका। जब ए० के० चोपड़ा उस महिला कर्मचारी की लज्जा भंग करने के लिये बेताब हो गया तो उस महिला कर्मचारी को विवश होकर उसके विरुद्ध कौंसिल के सक्षम अधिकारी को शिकायत करनी पड़ी। इस शिकायत पर ए० के० चोपड़ा को दिनांक 18.8.1988 को निलम्बित कर दिया गया। उसे आरोप-पत्र दिया गया। उसके विरुद्ध जाँच चली और अन्ततः जाँच में ए० के० चोपड़ा के दोषी पाये जाने पर उसे दिनांक 28.6.1989 को सेवा से निकाल दिया गया।
ए० के० चोपड़ा ने सेवामुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें उसे असफलता मिली। इस पर कौंसिल द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने दस्तक दी गयी। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने यह पाया कि ए० के० चोपड़ा द्वारा उस महिला कर्मचारी से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न मात्र किया गया लेकिन इन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुये थे। जब दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुये तो ऐसी स्थिति में ए० के० चोपड़ा को सेवा से मुक्त किया जाना उचित नहीं था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इसे लज्जा भंग का मामला नहीं माना फिर भी यह तो पाया कि वह महिला कर्मचारी ए० के० चोपड़ा की एक अधीनस्थ कर्मचारी थी। वह महिला कर्मचारी डिक्टेशन लेने में समर्थ नहीं थी फिर भी उसे डिक्टेशन लेने के लिये विवश किया गया और ताज पैलेस होटल में बुलाया गया। उस महिला कर्मचारी द्वारा वार-बार विरोध किये जाने के बावजूद भी ए० के० चोपड़ा ने उस महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। ए० के० चोपड़ा ने दुर्भावनापूर्वक आशय से बार-बार उस महिला कर्मचारी के पास बैठने का एवं निकट आने का प्रयास किया। ए० के० चोपड़ा अपनी इन हरकतों को बार- बार दोहराता रहा। इन सभी हरकतों से उस महिला कर्मचारी को क्षोंभ कारित हुआ तथा उस कार्यालय का वातावरण दूषित हुआ। पर इन सबके बावजूद भी चूँकि ए० के० चोपड़ा और उस महिला कर्मचारी के बीच शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया था इसलिये ए० के० चोपड़ा को सेवा से मुक्त कर दिया जाना उचित नहीं था।
उच्चतम न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने द्वारा विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिये गये निर्णय का अवलोकन किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना संविधान के भाग तीन में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हमारा संविधान लैंगिक समता की व्यवस्था देता है। पुरुष एवं स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया है। मात्र लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 21 में पुरुष एवं महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। इस सबके बावजूद भी यदि कोई पुरुषकर्मी कामकाजी महिला के साथ यौन उत्पीड़न कारित करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही यह महिला के सम्मान व गरिमा के विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि एक उच्च अधिकारी से अच्छे आचरण व व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कामकाजी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करे। इस प्रकरण में ए० के० चोपड़ा द्वारा उस महिला कर्मचारी के साथ जो कुछ भी किया गया वह क्षमा योग्य नहीं है।
ए० के० चोपड़ा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष शर्तरहित क्षमा याचना की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि यदि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है तो इससे कमकाजी महिलाओं का मनोबल गिरेगा। अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने कौन्सिल के निर्णय को सही ठहराते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया।
इस प्रकरण का पटाक्षेप तो इस तरह हो गया लेकिन घटना मानव समुदाय के समक्ष एकं ऐसा प्रश्न छोड़ गयी है जिस पर निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र सोच व चिन्तन की आवश्यकता है। बदलते हुए परिवेश में जहाँ महिलायें कर्म क्षेत्र में आने लगी हैं वहाँ उन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस प्रकार की घटनायें महिलाओं को प्रोत्साहित करने की बजाय निरुत्साहित हो करती हैं। अतः उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में न केवल एक सार्थक निर्णय है अपितु समय के दस्तावेज पर एक सशक्त हस्ताक्षर है।
प्रश्न 23. सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति के लिए दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए तथा किसी व्यक्ति को वेश्यागृह में निरुद्ध करने सम्बन्धी दण्ड की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर – सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार-
(1) वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की जायेगी-
(क) जो उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित कतिपय क्षेत्र या क्षेत्रों के अन्दर हों, या
(ख) जो किसी सार्वजनिक, धार्मिक पूजास्थल, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्यागृह या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर हों, जिसे पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट विहित रीति में इस निमित्त अधिसूचित करे,
कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।
(1-क) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी बालक या अवयस्क की बाबत है, वहाँ अपराध करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अन्यून की होगी किन्तु जो आजीवन कारावास के लिये या ऐसी अवधि के लिये जो दस वर्ष तक की हो सके, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :
परन्तु न्यायालय, पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के लिये कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।
(2) कोई व्यक्ति जो-
(क) किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिये जानबूझकर ऐसे स्थान में आश्रय लेने या वहाँ रहने देगा; या
(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का अभिधारी, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जानबूझकर उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने देगा; या
(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का स्वामी, पट्टाकर्ता या भू-स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टाकर्ता या भू-स्वामी का अभिकर्ता होते हुए उनको या उनके किसी भाग को जानते हुए पट्टे पर देगा कि उनका या उनके किसी भाग का वेश्यावृत्ति के लिये प्रयोग किया जाये अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा,
प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि सार्वजनिक स्थान या परिसर कोई होटल है तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारबार चलाने के लिये अनुज्ञप्ति तीन मास से अन्यून की अवधि के लिये किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, निलम्बित किये जाने के लिये दायित्व के अधीन होगी:
परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन किया गया कोई अपराध किसी होटल में किसी बालक या अवयस्क की बाबत है तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
(3) राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के किसी क्षेत्रों में किस प्रकार के व्यक्ति बार-बार आते-जाते हैं, और वहाँ के लोगों की प्रकृति कैसी है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुये; शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि वेश्यावृत्ति ऐसे क्षेत्र में नहीं की जायेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।
(4) जहाँ किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना में ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों की परिसीमायें युक्तियुक्त निश्चितता से परिनिश्चित करेगी।
(5) ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी जो जारी की जाने के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी तारीख से प्रभावी हो।
वेश्यावृत्ति के स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है (धारा 6) – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार-
(1) कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना –
(क) किसी वेश्यागृह में निरुद्ध करेगा; या
(ख) किसी परिसर में या पर इस आशय से निरुद्ध करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है, मैथुन करें,
दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अन्यून होगी तथा जो आजीवन के लिये या ऐसी अवधि के लिये जो दस वर्ष तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
परन्तु न्यायालय, पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के लिये कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा-
(2) जहाँ कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में किसी बालक के साथ पाया जाता है, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि उसने उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किया है।
(2-क) जहाँ किसी वेश्यागृह के अन्दर पाये गये किसी बालक या अवयस्क की चिकित्सीय परीक्षा पर उसके साथ लैंगिक दुरुपयोग किये जाने का पता चलता है, वहाँ जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि उस बालक या अवयस्क को, यथास्थिति, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये निरुद्ध किया गया है या उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये लैंगिक शोषण किया गया है।
(3) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वह किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या अपने विधिसम्मत पति से भिन्न किसी आदमी के साथ मैथुन के प्रयोजनों के लिये किसी परिसर में या उस पर निरुद्ध करता है, यदि ऐसा व्यक्ति, उसे वहाँ रखने के लिये विवश या उत्प्रेरित करने के आशय से-
(क) उसके किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य सम्पत्ति को उससे विधारित करता है, या
(ख) ऐसे व्यक्ति के द्वारा या निदेश से उसे उधार दिये गये या प्रदाय किये गये किसी आभूषण, पहनने के कपड़े, धन या अन्य सम्पत्ति को उसके द्वारा ले जाये जाने की दशा में उसे विधिक कार्यवाहियों की धमकी देता है।
(4) ऐसी स्त्री या लड़की के खिलाफ उस व्यक्ति के कहने पर जिसके द्वारा वह निरुद्ध की गयी है, किसी ऐसे आभूषण, पहनने के कपड़े या अन्य सम्पत्ति की वसूली के लिये जो ऐसी स्त्री या लड़की को उधार दी गयी है या प्रदाय की गयी अथवा ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा गिरवी रखी गयी अभिकथित है अथवा किसी धन की वसूली के लिये जिसका कोई स्त्री या लड़की द्वारा गिरवी रखी गयी अभिकथित है अथवा किसी धन की वसूली के लिये जिसका कोई स्त्री या लड़की द्वारा सन्देय होना अभिकथित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी प्रतिकूल विधि के होते हुए भी, नहीं होगी।
प्रश्न 24. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-
(1) व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना एवं उत्प्रेरित करना
(2) वेश्यावृत्ति के लिए याचना करने पर दण्ड
उत्तर (1) वेश्यावृत्ति के लिये किसी व्यक्ति को उपाप्त करने एवं उत्प्रेरित करने के लिए दण्ड – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति के लिये किसी व्यक्ति को उपाप्त करने आदि निम्न कृत्यों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है-
(i) किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से या सहमति के बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये उपाप्त करना या उपाप्त करने का प्रयत्न करना।
(ii) किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिये वेश्यागृह में जाने तथा वहाँ रहने के लिये उत्प्रेरित करना,
(iii) किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिये पालन-पोषण करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना या ले जाने का प्रयत्न करना,
(iv) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराना या करने के लिये उत्प्रेरित करना।
इन कृत्यों के लिये न्यूनतम तीन वर्ष तक तथा अधिकतम सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास एवं दो हजार रुपये तक के जुर्माने के लिये दण्ड की व्यवस्था की गयी है।
यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो अधिकतम कारावास की अवधि सात वर्ष की बजाय चौदह वर्ष तक की होगी।
यदि ऐसा कोई अपराध “बालक या अवयस्क” से सम्बद्ध है तो कारावास की अवधि क्रमशः न्यूनतम सात वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास तथा न्यूनतम सात वर्ष एवं अधिकतम चौदह वर्ष तक का कारवास होगी।
यदि किसी व्यक्ति के वेश्या के साथ पूर्व के सम्बन्ध उसे वेश्यावृत्ति कराने या उसके लिये उत्प्रेरित करने के रहे हैं तो यह इस धारा के अन्तर्गत अपराध के गठन के लिये पर्याप्त साक्ष्य होगी।
उत्तर (2) वेश्यावृत्ति के लिए याचना करने पर दण्ड- अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्यों को दण्डनीय अपराध माना गया है-
(i) किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई देते हुए और ऐसी रीति से जिससे दिखाई दे या सुनाई दे, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिये प्रलोभित करने हेतु-
(क) अंग विक्षेप करना,
(ख) शब्द उच्चारित करना, अथवा
(ग) शरीर का प्रदर्शन करना।
(ii) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति से-
(क) याचना करना,
(ख). छेड़छाड़ करना,
(ग) इर्द-गिर्द घूमना,
(घ) सार्वजनिक शिष्टता का अतिवर्तन करना जिससे अन्य व्यक्तियों को बाधा या क्षोभ कारित हो।
ऐसे अपराधों के लिये छः माह तक की अवधि के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पश्चात्वर्ती अपराध के लिये कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी एवं पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना भी देय होगा।
यदि ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा किया जाता है तो दण्ड की मात्रा न्यूनतम सात दिन का कारावास होगी जो तीन माह तक की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी अर्थात् कारावास की अधिकतम अवधि तीन माह तक की हो सकेगी।
प्रश्न 25. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए-
(क) वेश्यागृह
(ख) सुधार संस्था
(ग) वेश्यावृत्ति
(घ) वेश्या
(ङ) बालक
उत्तर (क)- वेश्यागृह – अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (क) के अनुसार-
“वेश्यागृह” के अन्तर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान अथवा किसी घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिये अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिये लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
उत्तर (ख)- सुधार संस्था- अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार-
“सुधार संस्था” से किसी नाम से ज्ञात कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है (जो धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है) जिसमें ऐसे व्यक्तियों को, इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, और इसके अन्तर्गत वह आश्रय स्थल भी है जहाँ विचारणीय व्यक्तियों को, इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, और इसके अन्तर्गत वह आश्रय- स्थल भी है जहाँ विचारणीय व्यक्तियों को अधिनियम के अनुसरण में रखा जाये।
उत्तर (ग)- वेश्यावृत्ति – अधिनियम की धारा 2 (च) में वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये लैंगिक शोषण या दुरुपयोग अभिप्रेत है। अर्थात्-
वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है- “किसी स्त्री द्वारा भाड़े के बदले में अपने शरीर को स्वच्छया मैथुन के लिये पेश करना।”
वेश्यावृत्ति स्वयं के शरीर को पेश करके अथवा किसी अन्य स्त्री या लड़की के शरीर को पेश करके की जा सकती है। इस प्रकार वेश्यावृत्ति स्वयं द्वारा की जा सकती है और किसी के द्वारा भी करायी जा सकती है।
उत्तर (घ) – वेश्या- वेश्या से अभिप्राय ऐसी स्त्री से है जो भाड़े के बदले मैथुन के लिये अपने शरीर को पेश करती है। वेश्या के लिये यह आवश्यक है कि वह-
(i) स्वेच्छया मैथुन के लिये,
(ii) धन के बदले में,
(iii) अपने शरीर को पुरुष के समक्ष अर्पित करे।
किसी भी स्त्री या लड़की को मात्र अपख्याति के आधार पर वेश्या नहीं कहा जा सकता है।
जैसे- यदि किसी महिला के घर रात्रि के समय काफी संख्या में पुरुष आते हों तो मात्र इस आधार पर उस महिला को वेश्या नहीं कहा जा सकता।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वेश्यावृत्ति में मैथुन के लिये शरीर का समर्पण धन या वस्तु के बदले में किया जा सकता है। आशय यह है कि प्रतिफल धन अथवा वस्तु कुछ भी हो सकता है।
उदाहरण-आराधना नाम की एक वेश्या एक पुरुष से 1500 रुपये लेकर अथवा घड़ी या चेन लेकर अपने आपको लैंगिक सम्भोग के लिये उस पुरुष को समर्पित करती है। यह “वेश्यावृत्ति” है और वह शरीर का समर्पण करने वाली वेश्या है।
उत्तर (ङ)- बालक- अधिनियम की धारा 2 (क) (क) के अनुसार ‘बालक’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
अध्याय 8
विवाह एवं विवाह-विच्छेद
(Marriage and Divorce)
प्रश्न 26. हिन्दू विधि में विवाह के स्वरूप का वर्णन कीजिए। Describe the Nature of Marriage in Hindu Law.
उत्तर- हिन्दू विधि में विवाह का स्वरूप – हिन्दू विधि विवाह को पवित्र एवं महत्वपूर्ण संस्कार मानती है। हिन्दू विधि में पुरुष पत्नी के बिना अधूरा समझा जाता है। पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। जैसा कि महाभारत के पर्व श्लोक संख्या 40-41 और 74 में बताया गया है कि वह व्यक्ति कौटुम्बिक जीवन बिताते हैं जिनकी पत्नियाँ होती हैं। जिनकी पत्नियाँ होती हैं वही व्यक्ति सुखी रह सकता हैं जिनकी पत्नियाँ होती हैं, वही पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और वही सम्यक् रूपेण अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मनमोहिनी बनाम बसन्त कुमार, (1909) 28 कलकत्ता 1752 के मामले में हिन्दू विवाह को मांस से मांस तथा हड्डी से हड्डी का मिलन बताया है। और इसे एक संस्कार से भी बढ़कर माना है। उच्चतम न्यायालय ने दुर्गा पी० बनाम अरुन्धती त्रिपाठी, (2005) 7 एस० सी० सी० 353 के मामले में यह मत व्यक्त किया कि विवाह स्वर्ग में तय होते हैं। हिन्दू विधि में विवाह को हिन्दुओं के 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार माना गया है। निम्नलिखित कारणों से हिन्दू विधि में विवाह को एक संस्कार माना गया है-
(1) पित्र ऋण की मुक्ति के लिए विवाह – प्रत्येक हिन्दू तीन ऋणों देव ऋण, ऋषि और पित्र ऋण के लिए दायी होता है। यज्ञ करके देव ऋण से, वेदाध्ययन करके ऋषि ऋण से और पुत्र उत्पन्न करके पित्र ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि पित्र ऋण से मुक्ति के लिए पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक और पुत्र की प्राप्ति पत्नी से होती है और पत्नी विवाह से मिलती है। इसलिए प्रत्येक हिन्दू के लिए विवाह अनिवार्य हो जाता है।
(2) स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विवाह- विवाह करने का दूसरा कारण परलोक की प्राप्ति और नरक से बचना है। हिन्दुओं में यह माना जाता है कि शूद्र वंश में पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हिन्दू विवाह का प्रमुख उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति होती है क्योंकि पुत्र श्राद्ध आदि कर्मों द्वारा पिता को नरक से बचाता है। जैसा कि मनु स्मृति में कहा गया है कि वही व्यक्ति पूर्ण पुरुष है जो पत्नी द्वारा सन्तान युक्त है।
(3) धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए विवाह – हिन्दू विधि पत्नी को धर्म पत्नी और पति की अर्धांगिनी मानती है। हिन्दू विधि के अनुसार बिना पत्नी के पुरुष अधूरा होता है। पत्नी पुरुष के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा कर देती है। धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के पूरे नहीं किये जा सकते हैं। अधिकतर धार्मिक अनुष्ठान पति-पत्नी गाँठ जोड़कर पूरा करते हैं।
(4) वंश वृद्धि के लिए विवाह – कुल को चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न होना आवश्यक होता है और पुत्र की प्राप्ति विवाह के बाद ही होती है। जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति (1-77) में कहा गया कि “स्त्री माता बनने के लिए स्वयं पुरुष पिता बनने के लिए उत्पन्न किये गये हैं।”
(5) विवाह न टूटने वाला एक बन्धन- हिन्दू विवाह जन्म-जन्मान्तर का साथ माना जाता है। कुछ स्मृतिकार तो विवाह को इतना पवित्र बन्धन मानते हैं कि उनके अनुसार विवाह का बन्धन मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। मनु के अनुसार कन्या का एक बार विवाह करने के बाद जीवनपर्यन्त वह उसी की बनी रहती है। यद्यपि नारद और पराशर निम्नलिखित 5 विशेष परिस्थिति में स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति देते हैं।
जब पति-
(1) लापता या खो गया हो,
(2) मर गया हो,
(3) सन्यासी हो गया हो,
(4) नपुंसक हो गया हो,
(5) जाति से निकाल दिया गया हो,
परन्तु उल्लेखनीय है उपर्युक्त प्रावधान केवल अमान्य विवाह पद्धतियों के लिए था, मान्य विवाह पद्धतियों के लिए नहीं। परन्तु अधिकांश स्मृतिकार दूसरे विवाह से असहमति व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार किसी भी परिस्थिति में दूसरा विवाह नहीं हो सकता। प्रसिद्ध स्मृतिकार मनु मनुस्मृति (अध्याय 5 श्लोक 157-158) में कहते हैं कि पति के मरने पर विधवा-पत्नी को फल-फूल पर जीवन यापन करते हुए शरीर को क्षीण कर लेना चाहिए परन्तु दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए। उसे इस प्रकार शरीर को क्षीण करते हुए ब्रह्मचारिणी का जीवन बिताते हुए मृत्यु तक सती का जीवन बिताना चाहिए।
(6) धार्मिक रीति से विवाह का किया जाना- हिन्दू विधि में विवाह अनुष्ठानों को सम्पन्न करके किया जाता है। पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। पुरोहित (द्विज) विवाह को सम्पन्न कराता है। कन्या और वर के द्वारा गाँठ जोड़कर पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी पूर्ण करने पर ही विवाह पूर्ण एवं वैध होता है। हिन्दू विवाह धार्मिक रीति से सम्पन्न न होने पर अपूर्ण माना जाता है।
(7) हिन्दू विवाह का संविदात्मक स्वरूप का न होना- हिन्दू विवाह संविदा की प्रकृति का नहीं होता क्योंकि संविदा के लिए जिन तीन अनिवार्य तत्वों प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल की आवश्यकता होती है। हिन्दू विवाह में इन तीनों का अभाव है अर्थात् हिन्दू विवाह में विवाह के पक्षकारों में मुस्लिम विवाह की तरह प्रस्ताव और स्वीकृति जैसी बात नहीं होती और न ही वर को दुल्हन प्राप्त करने के बदले में कोई प्रतिफल देना पड़ता है। कन्या का पिता स्वेच्छा से वर को कन्या दान में देता है। वह कन्यादान करने के बदले में कोई प्रतिफल नहीं लेता। इसके अतिरिक्त हिन्दू विवाह इस कारण से भी संविदा नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविदा के लिए पक्षकारों का वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक होता है। जबकि हिन्दू विवाह में पक्षकार अवयस्क एवं विकृतचित्त किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए हिन्दू विवाह को किसी भी दशा में संविदा तो कहा ही नहीं जा सकता।
उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि हिन्दू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है, संविदा नहीं।
विवाह का वर्तमान स्वरूप – हिन्दू विवाह का वर्तमान स्वरूप प्राचीन स्वरूप जैसा नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण अधिनियमों का पारित होना, सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कई अधिनियम पारित किये गये, जैसे हिन्दू विधवा विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम, 1956, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 हिन्दू विवाहित नारी का पृथक् आवास एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1946, हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1946, हिन्दू विधि मान्यता अधिनियम, 1941। परन्तु उपर्युक्त अधिनियमों के पारित होने के बावजूद जब अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पारित हुआ।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का हिन्दू विवाह पर प्रभाव- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिन्दू विवाह के स्वरूप को निम्नलिखित रूप से प्रभावित किया है।
(1) विवाह के सांस्करिक स्वरूप का प्रभाव – हिन्दू विवाह जो पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था, हिन्दू विधि मान्यता अधिनियम, 1955 के पारित होने के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस अधिनियम ने विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को पूर्णरूप से परिवर्तित कर दिया है अर्थात् हिन्दू विवाह का अब वह स्वरूप नहीं रह गया है जैसा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पी० वेंकटरमन बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1977 के मामले में बताया था कि “निःसन्देह हिन्दू विवाह धार्मिक संस्कार है। यही एक संस्कार स्त्रियों के लिए भी विहित किया है। यह एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह एक ऐसा बन्धन होता है जो अग्नि के सामने सप्तपदी पूर्ण करने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। इसे संविदा नहीं कहा जा सकता क्योंकि संविदा के लिए पक्षकारों का वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है जबकि हिन्दू विवाह के पक्षकार अवयस्क एवं विकृतचित्त कैसा भी हो सकता है।”
(2) वैवाहिक विधि पर प्रभाव – हिन्दू विवाह अधिनियम ने विधि में निम्नलिखित परिवर्तन करके प्राचीन हिन्दू विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को संविदात्मक स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया है-
(i) एक विवाह की मान्यता- अधिनियम ने बहुविवाह पर रोक लगा दी है और एक विवाह को विधि मान्यता प्रदान की है। दूसरा विवाह अपराध के रूप में दण्डनीय एवं शून्य घोषित किया गया है।
(ii) विवाह-विच्छेद का उपबन्ध अधिनियम ने विवाह के पक्षकारों को विवाह- विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण यहाँ तक कि पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद का उपचार प्रदान कर हिन्दू विवाह के प्राचीन स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है।
(iii) अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता अधिनियम ने अन्तर्जातीय विवाह को विधि- मान्य घोषित कर दिया है यहाँ तक कि हिन्दू के अर्थ के अधीन आने वाली जातियों के बीच सम्पन्न विवाह को वैधता प्रदान की गयी है।
(iv) विवाह की शर्तों का सरलीकरण- अधिनियम के अन्तर्गत सपिण्ड के विस्तार क्षेत्र को कम करके और प्रतिषिद्ध नातेदारों को सरलीकरण कर दिया गया है। सीमित करके हिन्दू विवाह की शर्तों का
(v) नये अनुतोषों का उपबन्ध।
(vi) शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को वैधता।
(vii) सगोत्र विवाह को विधिमान्यता।
(viii) विवाह-विच्छेद के बाद सन्तानों के भरण-पोषण एवं अभिरक्षा के बारे में व्यापक व्यवस्था ।
क्या विवाह का आधुनिक स्वरूप संविदात्मक है?
निम्नलिखित कारणों से यह कहा जा सकता है कि विवाह का आधुनिक स्वरूप संविदात्मक हो गया है-
(1) सहमति से विवाह विच्छेद की सुविधा – यद्यपि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में ही विवाह-विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण और विवाह को शून्य घोषित कराने की सुविधा प्रदान की गयी थी परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह विच्छेद करना आसान नहीं था। इसके अतिरिक्त विवाह विच्छेद की याचिका विवाह के 3 वर्ष पश्चात् ही की जा सकती थी। ऐसा उपबन्ध इसलिए किया गया था कि 3 वर्ष में विवाह पक्षकार ठीक से एक दूसरे को समझ लें। यदि कोई गलतफहमी हो गयी हो तो दूर कर लें। परन्तु संशोधन अधिनियम, 1976 ने यह उपबन्ध करके कि “विवाह पक्षकार आपसी सहमति से विवाह के एक वर्ष पश्चात् विवाह विच्छेद करवा सकते हैं। यदि विवाह के सांस्कारिक स्वरूप को चकनाचूर करके हिन्दू विवाह के स्वरूप को लगभग संविदात्मक कर दिया है।
(2) न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद के आधारों पर एकीकरण – विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 ने न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद के आधारों को एक कर दिया है। जिससे न्यायिक पृथक्करण की उपयोगिता समाप्त हो गयी है क्योंकि अब कोई पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करना इसलिए पसन्द नहीं फरता क्योंकि उसे उन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधारों के एकीकरण के उपबन्ध ने हिन्दू विवाह के स्वरूप को संविदात्मक स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्रदान की है।
(3) यौन सम्बन्धी बीमारी एवं मस्तिष्क विकृतता के आधार पर विवाह- विच्छेद- पहले यौन सम्बन्धी बीमारी और दिमागी विकृतता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री तभी प्रस्तुत की जाती थी जब कोई पक्षकार एक निश्चित अवधि 3 वर्ष से उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त होता था। परन्तु संशोधन अधिनियम, 1976 ने अवधि सम्बन्धी शर्तें समाप्त करके विवाह-विच्छेद को और आसान बना दिया है।
(4) जारता के आधार पर विवाह-विच्छेद- पहले जारता के आधार पर विवाह- विच्छेद की डिक्री पक्षकार के लगातार जारता में रहने पर मिलती थी इसके अतिरिक्त जारता को साबित करना बहुत कठिन था, परन्तु संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद अब जारता के एक ही कृत्य पर विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रदान की जा सकती है।
(5) विवाह पक्षकारों की आयु में परिवर्तन – बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1978 ने वरं और वधु की आयु सीमा बढ़ा दी है। अब विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष कर दिया है। इस परिवर्तन ने विवाह पक्षकारों को संविदा के लिए सक्षम पक्षकार बना दिया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अधिनियमों ने विवाह-विच्छेद को आसान बनाकर हिन्दू विवाह के इस प्राचीन सांस्कारिक स्वरूप को नष्ट कर डाला है, जिसे पति-पत्नी का जन्म-जन्मान्तर का कभी न समाप्त होने वाला रिश्ता माना जाता है।
अब उक्त अधिनियमों ने विवाह को संविदात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है और काफी हद तक अपने प्रयत्न में सफल भी हुए हैं परन्तु फिर भी हिन्दू विवाह को मुस्लिम विवाह की तरह संविदा नहीं कहा जा सकता। अतः हिन्दू विवाह को एक ऐसा विवाह कहा जा सकता है जो न तो पूर्ण रूप से सांस्कारिक रह गया है और न ही पूर्ण रूप से संविदात्मक ही रह गया है।
प्रश्न 27. वैध हिन्दू विवाह की आवश्यकं शर्तें क्या हैं? क्या एक हिन्दू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह कर सकती है?
What are essential conditions of valid Hindu Marriage? Can a Hindu girl marry with a Muslim boy?
उत्तर- वैध हिन्दू विवाह की आवश्यक शर्तें- हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5, विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करती हैं-
(1) एक विवाह
(2) मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना
(3) आयु
(4) प्रतिषिद्ध नातेदारी के अन्दर विवाह न होना
(5) विवाह के पक्षकारों का सपिण्ड न होना
(1) एक विवाह (धारा 5 (1) – अधिनियम की धारा 5 (1) यह अभिनिर्धारित करती है कि “विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी होनी चाहिए और न वधू का कोई जीवित पति होना चाहिए”।
स्वामीनाथन बनाम पलानी अम्मल एवं अन्य, ए० आई० आर० (2009) (एन० ओ० सी०) 221 मद्रास के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह करना धारा 5 (i) तथा (ii) के अधीन शून्य है परन्तु वहाँ दूसरे विवाह की इस आधार पर उपधारणा नहीं की जा सकती है कि दूसरे विवाह के पक्षकार एक साथ पति-पत्नी की तरह रहते हैं और समाज उन्हें पति-पत्नी के रूप में मान्यता देता है।
भोगड़ी कन्ना बाबू बनाम बुग्गिना पाइदम्मा, ए० आई० आर० (2006) सु० को० 2403 के मामले में एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से विवाह किया था। यह अभिनिर्धारित हुआ कि दूसरा विवाह शून्य था। परन्तु दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्रियाँ मृत पिता को सम्पत्ति की हकदार थीं।
पत्नी की सहमति से किया दूसरा विवाह वैध नहीं होता। भले ही पत्नी ने पति को दूसरा विवाह करने का अधिकार न्यायालय में वाद दायर करके घोषणा प्राप्त करने के बाद दिया हो। (श्रीमती सन्तोष कुमारी बनाम सुरजीत सिंह, ए० आई० आर० (1967) पटना 207]
(2) मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना [धारा 5 (2)] – विवाह की दूसरी शर्त है कि विवाह के पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ हों। अधिनियम की धारा 5 (2) निम्नलिखित व्यक्तियों को मानसिक रूप से स्वस्थ मानती हैं-
(i) विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न होना,
(ii) सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य न होना,
(iii) उन्मत्तता के दौरे से पीड़ित न होना।
यदि विवाह के पक्षकार को विवाह के समय दूसरे पक्ष की बीमारी के बारे में जानकारी हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में वर्णित विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है अर्थात् विवाह शून्यकरणीय नहीं होगा।
उच्चतम न्यायालय ने आर० लक्ष्मी नारायण बनाम शान्ती, (2001) सु० को० 854 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाह मानसिक अस्वस्थता के आधार पर वहाँ भी शून्य नहीं होगा जहाँ पति और पत्नी विवाह के पूर्व कई बार मिले हों और पति को पत्नी को समझने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। इस वाद के तथ्य निम्नलिखित थे- अपीलार्थी लक्ष्मण का विवाह 1.11.1987 को शान्ती के साथ हुआ था। 12 फरवरी, 1988 को लक्ष्मण ने विवाह को इस आधार पर अकृत एवं शून्य घोषित करने के लिए आवेदन किया कि शान्ती पुराने एवं असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित है। उसका कहना था कि विवाह की रात्रि में उसे सोते हुए पाया, उसने सहवास से मना कर दिया। उसने बताया कि वह बचपन से ही मानसिक रोग से ग्रस्त है और उसने विवाह पिता के दबाव में किया है। पति के आरोपों को पत्नी द्वारा इन्कार किया गया। उसका कहना था कि पति दहेज के लालच में दूसरा विवाह करना चाहता है। विचारण न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया। उच्च्च न्यायालय ने प्रथम अपील में पति के पक्ष में निर्णय दिया परन्तु द्वितीय अपील में पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया। पति द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। अपील खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय का मत था कि मानसिक अस्वस्थता के आधार पर धारा 12 (1) (ख) और 5 (ii) (ख) के अन्तर्गत विवाह को तभी अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है जब यह साबित किया जाये कि दूसरा पक्ष मानसिक रोग से. इस हद तक पीड़ित है कि उसके साथ सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करना असम्भव है।
(3) आयु (धारा 5 (3) – 1978 के पूर्व विवाह के समय वर को 18 वर्ष का और वधू को 15 वर्ष का होना आवश्यक था, परन्तु बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रवि कुमार बनाम दिल्ली राज्य, (2005) देलही एल० टी० आई० में कहा कि एक 15 वर्ष की लड़की अपनी शादी हेतु वैध सहमति देने के लिए स्वतन्त्र है।
परन्तु इस शर्त के उल्लंघन पर धारा 18 के अनुसार अपराधी पक्षकार को इसका दण्ड सादा कारावास 15 दिन तक का अथवा 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। किन्तु वर्तमान में इस सम्बन्ध में 2007 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 20 के द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 5 के खण्ड 3 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करेगा तो ऐसी शर्तों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास से अथवा 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
कोकुला सुरेश बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य, ए० आई० आर० (2009) आन्ध्र प्रदेश 52 के वाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बात की सम्पुष्टि की कि यदि अवयस्क कन्या का विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (3) के उल्लंघन में सम्पन्न किया गया है वहाँ ऐसा विवाह न तो शून्य होगा और न ही शून्यकरणीय होगा और उस स्थिति में विवाहिता का पति ही नैसर्गिक संरक्षक माना जायेगा न कि उसका पिता।
प्राचीन हिन्दू-विधि के अनुसार कन्या की विवाह योग्य आयु 8 वर्ष से 12 के अन्तर्गत होनी चाहिये तथा पुरुष की आयु 25 वर्ष के अन्तर्गत होनी चाहिये। किन्तु बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में जैसा कि 1949 ई० में संशोधित किया गया, विवाह के लिए आयु का निर्धारण पुनः किया गया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक तथा 15 वर्ष से कम आयु वाली कन्या के विवाह का निषेध कर दिया गया। जहाँ कन्या के संरक्षक की सहमति आवश्यक है। सहमति का प्रावधान अभिदेशात्मक था, जिसका अभाव फैक्टम वैलेट के सिद्धान्त द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। किन्तु जहाँ पक्षकारों के विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय तक स्वेच्छापूर्वक, पति-पत्नी ने ऐसा रहने का चयन कर लिया है, सहमति की आवश्यकता गौण मानी जाती थी।
(4) प्रतिषिद्ध नातेदारी के अन्दर विवाह न होना [धारा 5 (4)] – अधिनियम की धारा 5 (4) प्रतिषिद्ध नातेदारी (Prohibited Relationship) में आने वाले पक्षकारों के मध्य विवाह पर प्रतिबन्ध लगाती है।
“धारा 5 (4) जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों।”
(5) विवाह के पक्षकारों का सपिण्ड न होना [धारा 5 (5)]- अधिनियम की धारा 5 (5) सपिण्डों के बीच विवाह का प्रतिषेध करती है।
यदि विवाह के दोनों पक्षकारों के यहाँ कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा प्रचलित है जिसके कारण प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह और सपिण्डों में विवाह मान्य माना जाता है तो धारा 5 (4) और धारा 5 (5) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और मान्य होगा।
प्रश्न 28. “हिन्दू विवाह एक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा”। विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।
“Hindu Marriage is sacrament while Muslim marriage is contract.” Discuss. Mention decided cases.
उत्तर- यदि हम हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन करें तथा प्राचीन हिन्दू विधिशास्त्रों का अवलोकन करें तो हम पायेंगे कि हिन्दू विवाह समारोह हिन्दुओं के दस संस्कारों या शुद्धीकरण समारोहों में से अन्तिम संस्कार या समारोह है। हिन्दुओं में यह मान्यता है कि विवाह जन्म से पूर्व तय हो जाते हैं तथा उनको जन्म के पश्चात् मूर्त स्वरूप दिया जाता है तथा हिन्दू विवाह एक अटूट बन्धन है। प्राचीन हिन्दू मान्यता के अनुसार विवाह एक ऐसा सम्बन्ध है जो जन्म-जन्मान्तर तक चलता रहता है। कुछ स्मृतिकारों का तो यह कहना है कि हिन्दू विवाह एक धार्मिक तथा पवित्र बन्धन है जो एक पति या पत्नी के मध्य स्थापित होता है तथा मृत्यु भी इस बन्धन या सम्बन्ध को समाप्त नहीं कर सकती। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सम्माननीय न्यायाधीशों ने मनमोहिनी बनाम बसंत कुमार के बाद में हिन्दू विवाह को एक संस्कार से भी अधिक महत्व दिया है। यह माँस के साथ माँस का तथा हड्डियों के साथ हड्डियों का संयोग है। हिन्दुओं के अनुसार विवाह का उद्देश्य सन्तान प्राप्त करना तथा धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना है जबकि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य पति-पत्नी के मध्य अधिकार तथा कर्तव्यों को जन्म देना है तथा उनसे उत्पन्न सन्तान को वैधता प्रदान करना है।
हिन्दू विवाह में विवाह की पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि इसका दैवी स्रोत है तथा यह पूर्व निश्चित होता है। अतः हिन्दू विवाह के अन्तर्गत पति अपनी पत्नी को ईश्वर से प्राप्त करता है तथा यदि पत्नी वफादार रहे तो पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कर्तव्य है।
शिवनन्दी बनाम भगवान्धीम्मा, (1962) में मद्रास उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि हिन्दू विवाह इसलिए एक बन्धन है क्योंकि विवाह पवित्र अग्नि के चारों और सात फेरों (सप्तपदी) से पूर्ण होता है तथा धार्मिक बन्धन का सृजन करता है तथा धार्मिक बन्धन एक बार सृजित (निर्मित) हो जाने पर छूट नहीं सकता। यह मुस्लिम विवाह की भाँति संविदा नहीं है जहाँ पक्षकारों की सहमति अनिवार्य होती है।
गोपाल कृष्ण बनाम मिथिलेश कुमारी (1979) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि हिन्दू विधि के अन्तर्गत वैवाहिक संस्था एक सामाजिक विधिक संविदा न होकर एक संस्कार है।
प्राचीन हिन्दू विधि में स्त्रियों को सम्मान तथा आदर दिया जाता था। मनु ने कहा था-पिता, भाई, देवर, साले आदि द्वारा अपने कल्याण के लिए भी स्त्रियों को सम्मान तथा पूज्य भावं दिया जाना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है भगवान प्रसन्न रहते हैं तथा जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है किसी भी सांस्कारिक रीति के अनुष्ठानं का फल नहीं मिलता। प्राचीन हिन्दू विधि में विवाह विच्छेद या तलाक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सिर्फ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में ही कुछ आधारों पर विवाह-विच्छेदः प्राप्त करने का अधिकार विवाह के पक्षकारों को प्रदान किया गया है। हिन्दू विवाह एक ऐसा बन्धन माना गया था कि विवाह के पश्चात् पति या पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान एक दूसरे की उपस्थिति के अभाव में पूर्ण नहीं माने जाते थे। आज भी हिन्दू प्रथा के अनुसार प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण होने के लिए पति तथा पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है।
वैदिक नियमों से यह स्पष्ट है कि एक पुरुष कई पत्नियाँ रख सकता है परन्तु पत्नी को एक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी के लिए पति ईश्वर के समान है। पत्नी प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों तथा धार्मिक कर्मकाण्ड में अपने पति के साथ जुड़ी रहती है। मनु ने कहा है कि वैदिक काल में हिन्दू विवाह बन्धन की पवित्रता की घोषणा बारम्बार की गई है तथा आदर्श परिवार को निश्चिततापूर्वक कई बार मान्यता दी गई है। कई प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को पति की अर्धांगिनी अर्थात् आधा शरीर माना है। मनु ने तलाक तथा स्त्रियों के पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी है। पति को पत्नी के साथ एक माना गया है। पत्नी को न तो विग्रह द्वारा न किसी अन्य अन्तरण विधि द्वारा पति से पृथक् किया जा सकता है। हिन्दू विवाह में सिर्फ कुमारी कन्या का दान किया जाता है। अतः प्राचीन शास्त्रों में तलाक तथा विवाह-विच्छेद को कभी भी मान्यता नहीं दी गई है। नारद तथा कौटिल्य की रचनाओं में ही पुनर्विवाह का उल्लेख है, परन्तु उसका क्षेत्र बहुत सीमित है। इनके अनुसार लापता होने, मृत्यु हो जाने, संसार त्याग, नपुंसकता तथा उपेक्षा जैसी पाँच विपत्तियों में ही एक पत्नी दूसरा पति का वरण कर सकती है परन्तु मनु ने इस विचार का जोरदार विरोध किया है।
हिन्दू विवाह एक संस्कारपूर्ण बन्धन है। इसके कई अर्थ हैं। प्रथम तो स्त्री तथा पुरुष के मध्य विवाह एक धार्मिक तथा पवित्र बन्धन है, यह सिर्फ संविदात्मक बन्धन नहीं है। हिन्दुओं के लिए विवाह एक उत्तरदायित्व है जिसका उद्देश्य अपने पूर्वजों के ऋण को चुकता करने हेतु पुत्र पैदा करना नहीं है परन्तु यह कि पुत्र पैदा करने का उद्देश्य पुत्र द्वारा किए जाने वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना है।
शास्त्रों के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें एक कन्या को सुयोग्य व्यक्ति को दान में देकर पिता पर अधिरोपित धार्मिक तथा पवित्र कर्तव्य का निर्वाह करना होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह से पिता को एक महान आध्यात्मिक लाभ मिलता है।
विवाह की परिभाषा – हिन्दू विवाह एक दीवानी संविदा नहीं है। इसी प्रकार हिन्दू विवाह ईसाई विवाहों की भाँति संविदा नहीं है। ईसाई तथा मुस्लिम विवाह प्रस्ताव तथा स्वीकृति के माध्यम से निर्मित होते हैं तथा निरस्त होते हैं। मुस्लिम विवाह से भी हिन्दू विवाह पृथक् है क्योंकि मुस्लिम विवाह की प्रकृति संविदात्मक होती है। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना तथा सन्तान को वैधता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने हेतु सन्तान उत्पत्ति करना नहीं होता। मुस्लिम विवाह में प्रस्तावना तथा स्वीकृति होती है तथा यह स्वतन्त्र होनी चाहिए। प्रस्तावना तथा स्वीकृति की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने हेतु साक्षियों या गवाहों की उपस्थिति भी होती है। काजी दोनों पक्षकारों से निकाह की स्वीकृति मौखिक रूप से सुनने के पश्चात् ही निकाह को वैधता देता है। दूसरे मुस्लिम विवाह में प्रतिफल (मेहर) का होना आवश्यक है। जैसे-संविदा में प्रतिफल के बिना संविदा शून्य होती है उसी प्रकार मुस्लिम विवाह भी मेहर के अभाव में शून्य होता है। यह मेहर निश्चित या अनिश्चित, तुरन्त भुगतान या विलम्बित भुगतान के रूप में हो सकती है। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य भी सन्तान को वैधता प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ भी धार्मिक नहीं होता। मुस्लिम विवाह को संविदा की भाँति विच्छेद करना, खण्डित करना भी आसान है। इसके विपरीत हिन्दू विवाह में एक पिता अपनी कुँवारी कन्या को सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप कर अपने आध्यात्मिक या धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने का उद्देश्य रखता है जिससे उसे धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। हिन्दू विवाह का उद्देश्य सन्तान को सिर्फ वैधता प्रदान करना नहीं होता है अपितु इस विवाह का उद्देश्य यह होता है कि पिता अपनी मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक कर्मकाण्डों को पूरा करने हेतु एक सन्तान उत्पन्न करे जिसके द्वारा समस्त धार्मिक कर्मकाण्डों में पिता को धार्मिक लाभ मिलेगा।
हिन्दू विवाह एक संस्कार है जो एक हिन्दू के लिए आवश्यक संस्कार है। विवाह के पश्चात् एक हिन्दू स्त्री अपने गोत्र का परित्याग करती है तथा अपने पति के गोत्र को अपना लेती है। यहाँ एक सम्बन्ध स्थापित होता है न कि भिन्न। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्कार पूरा करना होता है न कि सिर्फ आनन्द प्रमोद। हिन्दू विवाह एक पूर्व निश्चित सम्बन्ध होता है जो अविच्छिन्न माना जाता है। यह अवयस्कता के दौरान सम्पन्न होने के कारण अवैध नहीं हो जाता अतः हिन्दू विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान ही है।
यद्यपि हिन्दू विधि मान्यता अधिनियम, 1955 का संशोधन (बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1978) करके हिन्दू विवाह के पक्षकारों की उम्र (वर की उम्र 21 तथा वधू की उम्र 18) निश्चित कर दी गई फिर भी ग्रामीण अंचलों में तथा शहर में भी धार्मिक विचार वाले माता-पिता यथाशीघ्र अपनी पुत्री का विवाह कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 18 द्वारा निर्धारित उम्र से कम वर या वधू के विवाह कराने वालों पर दण्ड का प्रावधान किया गया है परन्तु इसे लागू करने में प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थिति यथावत् बनी हुई है।
प्रश्न 29. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-
(1) दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना
(2) न्यायिक पृथक्करण
Write short notes on the following-
(1) Restitution of conjugal rights
(2) Judicial separation
उत्तर (1) – दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन (Restitution of conjugal rights)- विवाह द्वारा पति-पत्नी पर एक दूसरे के साहचर्य और सहवास का दायित्व उत्पन्न होता है परन्तु यदि एक पक्षकार दूसरे के साथ रहने से इन्कार करता है तो क्या दूसरा पक्षकार इन्कार करने वाले पक्षकार को अपने साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। यहूदी विधि में दाम्पत्य अधिकारों में पुनः स्थापन अर्थात् इन्कार करने वाले पक्षकार का व्यथित पक्षकार के साथ-साथ दाम्पत्य सम्बन्ध पुनः स्थापित करने का प्रावधान था। यहूदी विधि से यह उपबन्ध अंग्रेजी विधि के माध्यम से हिन्दू विधि में भी आ गया। दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिक्री (आज्ञप्ति) का तात्पर्य है कि न्यायालय दोषी पक्षकार को निर्दोष पक्षकार के साथ रहने की आज्ञा देता है। प्रारम्भिक काल में इस आज्ञा का पालन प्रतिपक्षी की गिरफ्तारी करके याचिकाकार को सुपुर्द करके किया जाता था। इस समय यह उपचार पति को ही प्राप्त था क्योंकि पति का पत्नी पर दाम्पत्य अधिकार था। कुछ समय उपरान्त यह अधिकार पत्नी को भी प्राप्त हो गया तथा दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री को प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी द्वारा प्रवर्तित कराने का उपबन्ध समाप्त कर दिया गया। यद्यपि डिक्री अब भी विपक्षी की सम्पत्ति कुर्क करके लागू की जा सकती है। आधुनिक अंग्रेजी विधि में दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन के वैवाहिक उपचार को समाप्त कर दिया गया है।
भारतीय विधि के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापन की डिक्री को प्रतिपक्षी की सम्पत्ति कुर्क करके प्रवर्तित कराया जा सकता है (दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 21, नियम 32) l
हिन्दू विधि मान्यता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत जब पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से उचित कारण के बिना अलग कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन, अर्जी द्वारा कर सकेगा और न्यायालय इस अर्जी में किये गये कथन की सत्यता के बारे में तथा इस बारे में कि आवेदन को मंजूर न करने का कोई वैध आधार नहीं है इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर तद्नुसार दाम्पत्य अधिकारों का पुनःस्थापन, डिक्री द्वारा करा सकेगा।
इस प्रकार धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों को पुनःस्थापन की डिक्री प्राप्त करने हेतु तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।
1. यह कि प्रतिपक्षी युक्तियुक्त कारण के बिना साहचर्य से अलग हो गया है।
2. यह कि न्यायालय गाचिकाकार द्वारा याचिका में कथित बयानों की सत्यता के बारे में सन्तुष्ट है।
3. यह कि अनुतोष प्रदान करने के मार्ग में कोई अन्य बाधा नहीं है।
साहचर्य से अलग होना- साहचर्य से पृथक् होने का तात्पर्य याचिकाकार का साहचर्य बिना अनुमति या सहमति के छोड़ देना है। इस सम्बन्ध में भारतीय न्यायालयों के समक्ष एक प्रश्न यह खड़ा हुआ कि पति के आदेशानुसार पत्नी का अपनी नौकरी या कार्य को न छोड़ना क्या साहचर्य से चर्य से अलग होने की कोटि में आयेगा। तीरच कौर बनाम कबाल सिंह के बाद में पत्नी को पतिगृह से दूर एक नौकरी मिल गई। वह वहाँ रहने लगी। कभी-कभी पति भी उसके साथ जाकर रह लेता था। कुछ समय पश्चात् उनमें मन-मुटाव हो गया। पति ने पत्नी को नौकरी त्याग कर अपने पास रहने रहने का आदेश दिया। पत्नी ने अपने लिखित कथन में कहा कि वह पति के साथ सहवास करना चाहती है परन्तु नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि संसार की किसी भी विधि के अन्तर्गत पत्नी अपने पति के साहचर्य से इस भाँति विलग नहीं हो सकती अर्थात् पति अपनी पत्नी को नौकरी त्याग कर अपने साथ रहने के लिए विवश कर सकता है।
परन्तु गया प्रसाद बनाम भगवती, (1965) में इसी प्रकार के तथ्य पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि हिन्दू समाज की सामान्य मान्यताओं के अनुसार पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने दाम्पत्य उत्तरदायित्व पतिगृह में रहकर पूरे करे और वह पति से पृथक् घर बसाकर रहने की अपनी एकतरफा इच्छा को पति पर यह कहकर नहीं थोप सकती कि उसे उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि जहाँ वह नौकरी करती हो उसका पति उसके साथ आकर रहे। न्यायमूर्ति श्री भार्गव ने कहा कि पत्नी का यह आचरण अभित्यजन की संज्ञा में आता है।
परन्तु उपरोक्त निर्णय के विपरीत मत तीरथ कौर के वाद (1975) में रेवेन्यू लॉ रिपोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्त्री पुरुष के बीच नियोजन के अनुसार हो समानता के इस युग में पत्नी द्वारा नौकरी करने तथा पति के आदेश पर उसे न छोड़ने को साहचर्य से अलग हो जाना नहीं कहा जा सकता। रमेश (1972) के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति काटजू ने कहा कि पति के निर्देश पर पत्नी द्वारा अपने पद से त्याग पत्र न देना दाम्पत्य अधिकारों की डिक्री देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तथा यदि पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध भी नौकरी या अन्य कोई कार्य करे तो यह साहचर्य से विलग होना नहीं कहा जायेगा तथा दाम्पत्य अधिकारों को पुनः स्थापना का आधार नहीं बनेगा। राधाकृष्णन बनाम धनलक्ष्मी (1975) में मद्रास उच्च न्यायालय, मिजूमल बनाम देवी (1977) में उच्च न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया तथा यही मत सही है। राजस्थान उचित कारण क्या है, इसके विषय में कठोर सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर होगा।
(व) क्या दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना का अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है- आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष टी० सरीथा बनाम वेंकट सुब्बैया, ए० आई० आर० (1983) ए० पी० 356 में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापन का अधिकार संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
डी० सरीथा बनाम सुब्बैया, ए० आई० आर० 1983 ए० पी० 356 के बाद में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनःस्थापन का अधिकार के उपचार घृणित, क्रूर, असभ्य, नृशंस तथा अमानवीय हैं तथा यह व्यक्ति के मान व मर्यादा और एकांतता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इस अनुतोष से नारी की इस स्वतन्त्रता का हनन होता है कि कब, किस समय तथा किस प्रकार वह गर्भ धारण करके सन्तानोत्पत्ति करना चाहेगी। पुनःस्थापन की डिक्री से राज्य उसे उसकी इच्छा के विपरीत गर्भाधान करने के लिए बाध्य करती है अतः यह उपचार असंवैधानिक है।
इसके विपरीत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवध बिहारी रोहतगी के अनुसार हरविन्दर कौर बनाम हरमन्दर सिंह चौधरी, (ए० आई० आर० 1984 दिल्ली 66) दाम्पत्य अधिकारों का पुनःस्थापन का उपचार विवाह के पक्षकारों के बीच मतभेद समाप्त कर उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाता है।
सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, ए० आई० आर० 1984 एस० सी० 1562 के बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सव्यसाची मुखर्जी ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन का उपचार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि आज दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन की डिक्री को प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसकी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है तथा यह उपचार पति तथा पत्नी को एक साथ रहने को प्रोत्साहित करता है, उनके विवाह को टूटने से रोकता है।
परन्तु यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यदि पति-पत्नी के मध्य सम्बन्ध कटुता की इस सीमा तक पहुँच चुके हों कि उन्हें पुनःस्थापित करने में किसी पक्ष को बाध्यता हो तो तनाव एवं कटुतापूर्ण जीवन व्यतीत करने से बेहतर होगा कि उनमें सम्बन्ध विच्छेद हो जाये।
उत्तर (2) – न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) वैसे तो पति-पत्नी दोनों का ही पवित्र कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को साहचर्य प्रदान करें परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब पति-पत्नी का एक साथ रहना सम्भव नहीं रह जाता। अधिनियम की धारा 10 ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण का उपबन्ध करती है। धारा 10 यद्यपि उन आधारों को नहीं बताती जिनके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की जा सकती है परन्तु धारा 10 (1), धारा 13 में वर्णित विवाह-विच्छेद के आधारों को ही न्यायिक पृथक्करण के आधार बताती है क्योंकि विवाह-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद के आधार एक ही हो गये हैं।
निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर पति-पत्नी कोई भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं-
(1) जारता या व्यभिचारिता का आचरण- जब किसी पक्षकार ने पति अथवा पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से लैंगिक संभोग किया हो।
(2) क्रूरता – जब याची के प्रति दूसरे पक्षकार ने क्रूरता का व्यवहार किया हो।
(3) अभित्याग- जब दूसरे पक्षकार ने याचिका प्रस्तुत किये जाने के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष से लगातार अभित्याग किया हो।
(4) धर्म परिवर्तन – जब दूसरा पक्षकार धर्म परिवर्तन के कारण हिन्दू न रह गया हो।
(5) विकृतचित्तता- जब दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृतचित्त रहा हो अथवा निरन्तर या बार-बार इस सीमा तक विकृतचित्त रहा हो कि आवेदक प्रत्यर्थी के साथ युक्तियुक्त रूप से नहीं रह सकता।
(6) कोढ़ (Leprosy) – जब याचिका प्रस्तुत किये जाने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्षकार उग्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा हो।
(7) संचारी रतिजन्य रोग (Communicable Veneral Disease)- जब दूसरा पक्षकार इस प्रकार के रतिजन्य रोग से पीड़ित रहा हो जो सम्पर्क से दूसरे को भी हो सकता है।
(8) सन्यासी होना- जब दूसरे पक्षकार ने किसी धार्मिक पन्थ के अनुसार सन्यास ग्रहण कर लिया हो।
(9) सात वर्ष से लापता होना- न्यायिक पृथक्करण की डिक्री तब भी प्राप्त की जा सकती है जब विवाह का दूसरा पक्षकार सात वर्ष या उससे अधिक अवधि से उन लोगों द्वारा जीवित न सुना गया हो जिन लोगों द्वारा यदि वह जीवित होता तो सुना जाता।
न्यायिक पृथक्करण का परिणाम –
न्यायिक पृथक्करण को डिक्री प्राप्त कर लेने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं-
1. सहवास के दायित्व से मुक्ति- यद्यपि न्यायिक पृथक्करण से वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त नहीं होते परन्तु याची प्रत्युत्तरदाता के साथ सहवास के दायित्व से मुक्त हो जाता है। परन्तु पक्षकार यदि चाहें तो पति-पत्नी के रूप में रह सकते हैं।
2. पुनर्विवाह करने पर प्रतिबन्ध – न्यायिक पृथक्करण के दौरान विवाह का कोई पक्षकार पुनर्विवाह नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ जारकर्म कर सकता है क्योंकि यदि विवाह का कोई पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के साथ जारकर्म करता है तो विवाह का दूसरा पक्षकार विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है।
3. मूल विवाह अस्तित्वहीन नहीं होता- न्यायिक पृथक्करण से विवाह का अस्तित्व अप्रभावित रहता है- यदि पक्षकार चाहें तो वे बिना पुनः विवाह संस्कार को सम्पन्न किए ही पुनः वैवाहिक जीवन प्रारम्भ कर सकते हैं।
4. एक वर्ष तक सहवास न होने पर विवाह-विच्छेद- जब, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के 1 वर्ष बाद तक विवाह के पक्षकार पुनः सहवास प्रारम्भ नहीं करते तो वह विवाह- विच्छेद का आधार हो जाता है।
क्या यह परिवर्तन हिन्दू समाज की आवश्यकता के अनुकूल है?
हाँ, न्यायिक पृथक्करण में सन् 1976 में जो संशोधन किये गये वह हिन्दू समाज की आवश्यकता के अनुकूल है। लेखक के अनुसार, “हिन्दू विवाह एक संस्कार होता है जिसमें विवाह का बंधन अटूट माना जाता है, बात-बात में विवाह विच्छेद नहीं हो जाता। अतः हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा न्यायिक पृथक्करण द्वारा उन्हें एक ऐसा मौका मिले ताकि वे फिर से मिल सकें इसलिए इसमें केवल वैवाहिक सम्बन्ध स्थगित रहता है टूटता नहीं और समागम के बाद पुनः पहले जैसे पति-पत्नी की अवस्था में आ जाते हैं।” अतः यह व्यवस्था लेखक के मतानुसार हिन्दू समाज के अनुकूल हैं।