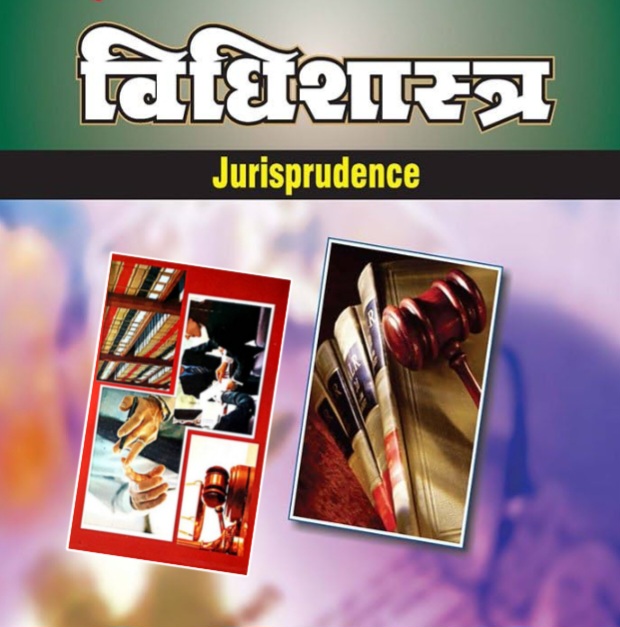-: लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर :-
प्रश्न 1. “विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है।” टिप्पणी कीजिए। “Jurisprudence is the Science of Law”. Comment.
उत्तर – प्रसिद्ध विधिशास्त्री ‘सामण्ड’ महोदय ने अपनी पुस्तक ‘जूरिसडेन्स में विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि “विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है।’ (Jurisprudence is the Science of Law) विधि से उसका तात्पर्य है देश की विधि या देशीय विधि (Civil Law)। इस अर्थ में तीन प्रकार सामने आते हैं-
(1) व्याख्यात्मक – जो ऐसी किसी वास्तविक विधि की प्रणाली के तत्वों का विवेचन करता है, जो कि किसी समय मौजूद हो, चाहे भूतकाल में या वर्तमान में।
(2) विधिक इतिहास – जो किसी विधि प्रणाली के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का विवेचन करता है।
(3) विधान विज्ञान- इसका प्रयोजन ऐसी विधि बनाना है जैसी कि यह होनी चाहिए। यह विधि – प्रणाली के आदर्श भविष्य और उन प्रयोजनों का जिनके लिए इसका अस्तित्व होता है, वर्णन करता है।
सामण्ड ‘विधिशास्त्र’ शब्द का ‘सामान्य’ और ‘विशिष्ट’ में भेद करता है। पहले के अन्तर्गत विधि सिद्धान्तों का सम्पूर्ण समूह आता है, जबकि दूसरे का अभिप्राय ऐसे सिद्धान्तों के एक विशिष्ट विभाग से होता है। दूसरे अर्थ में इसको सैद्धान्तिक या ‘सामान्य’ विधिशास्त्र कहा जा सकता है। सामण्ड कहता है कि उसकी पुस्तक केवल उस विधिशास्त्र से सरोकार रखती है जिसे वह ‘सिविल विधि के मूल सिद्धान्तों का विज्ञान’ (The Science of the first principles of civil law) कहकर परिभाषित करता है।
प्रश्न 2. “विधिशास्त्र विधि का नेत्र है”। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। “ Jurisprudence is the eye of law”. Write short notes.
उत्तर– सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री ‘लॉस्की’ महोदय ने अपनी पुस्तक में विधिशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा कि “विधिशास्त्र विधि का नेत्र है” (Jurisprudence is the eye of law) जिस प्रकार मानव शरीर में यदि नेत्र न हो तो उस व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण संसार अंधकारमय है उसी प्रकार यदि विधि में विधिशास्त्र न हो तो विधि का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।
अतः किसी भी राष्ट्र की विधि तभी सर्वांगीण विकास करती है जब वहाँ विकसित विधिशास्त्र मौजूद रहता है। बिना विधिशास्त्र के विधि के अस्तित्व की कल्पना करना एक कोरी कल्पना मात्र है। अतः हम कह सकते हैं कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, क्योंकि इससे नागरिकों को कानून का ज्ञान, अवहेलना पर दण्ड व विधियों से होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है।
प्रश्न 3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिन्दु है। स्पष्ट करें। International Law is the vanishing point of Jurisprudence. Explain.
उत्तर- चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वतन्त्र तथा सम्प्रभु राष्ट्रों के सम्बन्धों तथा क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने के नियमों का समूह है, अतः इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई स्वतन्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि को मानने से इन्कार कर दे तो उसके विरुद्ध क्या उपाय है? दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को बाध्यकारी मानने से इंकार करने वाले सम्प्रभु तथा स्वतन्त्र राष्ट्र के विरुद्ध कोई बाध्यकारी उपाय इस विधि में न होने के कारण यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में या यथार्थ में विधि है। इसकी बाध्यता शक्ति क्या है?
ऑस्टिन ने यह कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि नहीं है बल्कि यह आचरण सम्बन्धी नियमों की संहिता है जिसे केवल नैतिकता का ही बल प्राप्त है तथा इसमें अपने से वरिष्ठ की आज्ञा के समान बाध्यकारी बल की कमी है।
हॉल्स तथा वुफेन डार्फ नामक विधिशास्त्रियों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वाटेल नामक विधिशास्त्री ने तो यहाँ तक कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि मूल में कुछ नहीं वरन् प्रकृति के नियम हैं जो राष्ट्रों पर लगाये गये है। हॉलैण्ड के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से इस बात से भिन्न है कि इसे राज्य की प्राधिकारपूर्ण शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लोपकारी बिन्दु (Vanishing Point of Jurisprudence) है।
प्रश्न 4 “विधि दमन का एक साधन है” व्याख्या कीजिए। Explain “Law is the instrument of suppression”.
उत्तर – विधि दमन का एक साधन है— मॉर्क्स के अनुसार, विधि उसे प्रस्तुत करती है जिसे ऊपरी ढाँचा कहा जाता है। यह बुर्जुआ पूँजीवादी प्रणाली में आर्थिक रूप से प्रभुताशाली और शोषक वर्ग के हितों को प्रोलेतेरियत (Proletariat ) अर्थात् दलित वर्ग की कीमत पर आगे बढ़ाने को कारगर करने के लिए होती है।
विधि पर मार्क्सवादी विचार के विस्तृत क्षेत्र को टंट द्वारा संक्षेप में छः शीर्षकों में रखा गया है-
(1) विधि अपरिहार्य रूप से राजनीतिक है अथवा विधि राजनीति का रूप है।
(2) विधि और राज्य घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं, विधि राज्य से एक सापेक्ष स्वायत्तता प्रकट करती है।
(3) विधि दर्पण को प्रभावी करती है अथवा अन्यथा विद्यमान आर्थिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है. विधिक प्रणाली, आर्थिक सम्बन्धों की प्रणाली की प्रतिकृति होती है।
(4) विधि सर्वदा सम्भाव्य प्रपीक अथवा दमनात्मक होती है और प्रपीड़न के साधनों के राज्य के एकाधिकार को प्रकट करती है।
(5) विधि की विषयवस्तु और प्रक्रिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुताशाली वर्ग या शक्ति गुट के हितों को प्रकट करते हैं।
(6) विधि आदर्शात्मक होती है, यह प्रभुताशाली वर्ग के अन्तर्भूत मूल्यों का नमूना होने और उन्हें विधिमान्यता प्रदान करना दोनों काम करती है।
प्रश्न 5. सामण्ड द्वारा दी गयी विधिशास्त्र की परिभाषा पर एक टिप्पणी लिखिए। Write a note on Salmond’s definition of Jurisprudence.
उत्तर- सामण्ड की परिभाषा (Salmond’s Definition )–सामण्ड ऑस्टिन तथा हालैण्ड के इस विचार को मान्यता देते हैं कि विधिशास्त्र एक विज्ञान है। परन्तु सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र सामान्य न होकर विशिष्ट (Particular) है। विशिशास्त्र एक विशिष्ट विधि व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों का अध्ययन है। सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र विधि की एक विशिष्ट शाखा का अध्ययन है जिसे सिविल या नागरिक विधि कहते हैं। सामण्ड विधिशास्त्र को एक विशिष्ट अधिरचित (सकारात्मक) विधि पद्धति के सन्दर्भ में परिभाषित करते हैं। सामण्ड के अनुसार विधिशास्त्र नागरिक विधि या दीवानी विधि (Civil Law) के प्रथम सिद्धान्तों का विज्ञान (Science of first Principle of civil law) है। “प्रथम सिद्धान्त” शब्द से सामण्ड का तात्पर्य किसी विशिष्ट विधि के मौलिक सिद्धान्तों (Fundamental Principles) से है। किसी विधि पद्धति के मौलिक सिद्धान्त उस विधि पद्धति के गौण विधिक नियम (Subsidiary legal rules) या सिद्धान्तों से भिन्न है। सामण्ड यह स्वीकार करते हैं कि किसी विधि पद्धति के मौलिक सिद्धान्त तथा उस विधि के गौण नियम के मध्य विभाजन रेखा खींचना कठिन कार्य है। प्रथम सिद्धान्त तथा अवशिष्ट विधि में अन्तर स्तर (degree) का है न कि प्रकार (Kind) का। मौलिक सिद्धान्तों को परिभाषित करते हुए सामण्ड कहते हैं कि मौलिक सिद्धान्त वे मौलिक परकिल्पनाएँ तथा सिद्धान्त हैं जो किसी विधि के ठोस विवरण का आधार होती हैं। विधिशास्त्री को विधिशास्त्र में किसी नागरिक विधि के मौलिक सिद्धान्तों के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। विधिशास्त्र में किसी विधिक पद्धति के अवशिष्ट विधि के सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं होना चाहिए।
प्रश्न 6. ‘विध्यात्मक विधि’ से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Positive Law”?
Or
“विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है” स्पष्ट करें। ” Jurisprudence is the formal science of Positive Law” Explain.
उत्तर- प्रसिद्ध विधिशास्त्री हॉलैण्ड ने विधिशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि ” विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है।” (Jurisprudence is the formal Science of Positive Law)। प्रारूपिक विज्ञान से उसका तात्पर्य उससे है जो उन विभिन सम्बन्धों से मतलब रखता है जो स्वयं उन सम्बन्धों को विनियमित करने वाले नियमों की अपेक्षा विधिक नियमों से विनियमित होते हैं।
हॉलैण्ड विध्यात्मक विधि की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि विधिशास्त्र कारण कार्य के रूप में ऐसे विधिक सम्बन्धों का विज्ञान नहीं है जैसे वे होते या होने चाहिए, किन्तु यह ऐसे सम्बन्धों से कार्य-कारण तर्क के रूप में निकलता है जिनका वास्तविक प्रणाली में एक विधिक स्वरूप होता है। दूसरे शब्दों में विध्यात्मक विधि का अर्थ वस्तुतः विद्यमान विधि है। जो आदर्श विधि अथवा विधि क्या होनी चाहिए से भिन्न है।
हॉलैण्ड की इस परिभाषा की ग्रे महोदय, एडवर्ड जैक्स, प्रो० एडम्सन आदि विधिशास्त्रियों ने आलोचना की। प्रो० ग्रे ने औपचारिक शब्दों के कारण हॉलैण्ड की परिभाषा को संकीर्ण एवं अस्पष्ट बताया है। डॉ० एडवर्ड जैक्स ने भी औपचारिक शब्द पर हॉलैण्ड की परिभाषा की कटु आलोचना की है। उन्होंने कहा कि औपचारिक शब्द का प्रयोग करके हॉलैण्ड ने विधिशास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है, विषय पर नहीं।
प्रश्न 7. सम्प्रभुता से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Sovereignty.
उत्तर – सम्प्रभुता (Sovereignty) – ‘प्रभुता’ शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द सॉवरेन से हुई है जिसका तात्पर्य ऐसी सर्वोच्च शक्ति से से है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति न हो। कोई भी प्रभुतासम्पन्न राज्य किसी अन्य के अधीन नहीं होता उस राज्य के सभी व्यक्ति प्रभुतासम्पन्न की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रभुतासम्पन्न राज्य बाह्य नियन्त्रणों से पूर्णतः मुक्त रहता है। ऑस्टिन ने प्रभुता सम्पन्न की शक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त में प्रभुता की तीन विशेषताओं को बतलाया है-
(1) प्रभुता की अनिवार्यता,
(2) प्रभुता की अविभाज्यता,
(3) प्रभुता की असीमितता ।
प्रश्न 8. सम्प्रभुता की प्रमुख विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। Write a note on main characteristics of Sovereignty.
उत्तर-सम्प्रभुता की प्रमुख विशेषताएँ – ऑस्टिन ने प्रभुता सम्पन्न की शक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त में प्रभुता की तीन विशेषताओं को बतलाया है-
(1) प्रभुता की अनिवार्यता – ऑस्टिन का मत है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोपरि शक्ति अवश्य होती है। यह प्रभुता शक्ति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक समूह में निहित हो सकती है तथापि यह आवश्यक नहीं है कि प्रभुता राज्य के भीतर ही निहित हो। वह आंशिक रूप से या पूर्णतः राज्य के बाहर भी हो सकती है।
(2) प्रभुता की अविभाज्यता- प्रत्येक राज्य में केवल प्रभुता शक्ति का होना मात्र पर्याप्त नहीं है बल्कि उसमें प्रभुताधारी भी होना चाहिए, अर्थात् राज्य में एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसमें प्रभुताशक्ति निहित हो।
(3) प्रभुता की असीमितता – विधिक दृष्टि से प्रभुता असीमित होती है अर्थात् प्रभुतासम्पन्न राज्य बाह्य तथा आन्तरिक नियन्त्रणों से मुक्त रहता है, अर्थात् उसकी वैधानिक शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 9.विधिशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है? What is the importance of the stuty of Jurisprudence.
उत्तर- विधिशास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न कानूनों सम्बन्धी अवधारणाओं की विवेचना की जाती है जिनमें अधिकार, दायित्व, स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य, वैधानिक व्यक्तित्व, आशय, उपेक्षा आदि के सामान्य एवं व्यापक स्वरूप का निरूपण किया जाता है। विधिशास्त्र के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं-
(1) यह हमें विधि की प्रकृति का बोध कराता है। यह विधि के वास्तविक नियमों के अध्ययन और उनके आधारभूत सिद्धान्तों का अन्वेषण करने में सहायता करता है।
(2) यह विधि का वैज्ञानिक विकास करने में सहायक होता है।
(3) यह मस्तिष्क की आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करता है और विधिक अभिव्यक्तियों और शब्दावलियों का उचित बोध कराता है।
(4) विधिशास्त्र पर शोधों का समकालीन सामाजिक, राजनीतिक चिन्तन पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही वे भी उनके आदर्शों से प्रभावित हो सकते हैं।
(5) विधिशास्त्र विधिक संकल्पनाओं (Concepts) को तर्कयुक्त बनाने (rationalise) वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में हमें समर्थ बनाता है।
(6) विधिशास्त्र का शिक्षात्मक (Educational) मूल्य भी है। विधिक संकल्पनाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण विधिज्ञों के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता है और उनकी तर्क तकनीक को प्रखर बनाता है। यह उनकी वैयक्तिकता (individuality) और औपचारिकतावाद (Formalism) को दूर करने में सहायक होता है और उन्हें सामाजिक यथार्थों और विधि के कृत्यात्मक (Functional) पहलू पर केन्द्रित करने को प्रशिक्षित (Trained) करता है।
(7) विधिशास्त्र किसी निर्दिष्ट समाज में विधि के बुनियादी विचारों और सिद्धान्तों पर प्रकाश डालता है।
प्रश्न 10. ऑस्टिन द्वारा दी गयी विधिशास्त्र की परिभाषा को समझाइए। Discuss the definition of Jurisprudence given by Austin.
उत्तर-आस्टिन की परिभाषा – ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र सकारात्मक (Positive) या अधिरचित (Enacted) विधि का विश्लेषण (analysis) है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा कि विधाशास्त्र अधिरचित विधि (ऐसी विधि जो संसद या विधायिका द्वारा पारित विधि है) का विश्लेषण है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को सकारात्मक (अधिरचित : Enacted) या Positive (पॉजिटिव) विधि के दर्शन (Phylosophy) के रूप में परिभाषित किया। ऑस्टिन के अनुसार विधि का अध्ययन या विधि का विश्लेषण विधि के उद्देश्यों या विधि पारित करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए (What law ought be) परन्तु विधि का अध्ययन अधिनियम के अन्तर्गत निहित विधि हो है। विधि जैसी है (Law as it is) ही, विधि के अध्ययन या विश्लेषण या निर्वचन (Interpretation) की विषय-वस्तु है। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचित विधि (Positive Law) वह विधि है जिन्हें राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा राजनीतिक रूप से अवर व्यक्ति के लिए निरूपित किया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्रियों को विधि का अध्ययन करते समय विधि कैसी होनी चाहिए इससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए बल्कि विधि का अध्ययन विधि निरूपित है, वैसी ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पोस्टल अधिनियम में डाक कर्मियों की उपेक्षा के लिए निर्धारित प्रतिकर 500/- है तो न्यायाधीश अधिकतम 500/- रुपया प्रतिकर ही दिला सकता है। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह इस मामले में यह देखे कि डाक कर्मियों की उपेक्षा से कथित पक्षकार को कितनी क्षति हुई है। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र, विधि का नैतिक दर्शन (Moral phylosophy) नहीं है परन्तु विधिशास्त्र विद्यमान, वास्तविक तथा अधिरचित (सकारात्मक: Positive) विधि का वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध (सुव्यवस्थित) अध्ययन (विश्लेषण) है। ऑस्टिन विज्ञान का विद्यार्थी था अतः ऑस्टिन ने विधि के विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical study) पर अधिक बल दिया। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्रियों को विधि का उसी प्रकार विश्लेषण करना चाहिए जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी रासायनिक पदार्थ का विश्लेषण करता है। उसे रासायनिक पदार्थ के बाह्य परिवेश से कोई प्रयोजन नहीं है।
प्रश्न 11. रूडोल्फ स्टेमलर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। What a short note on Rudolf Stamler.
उत्तर- बीसवीं शताब्दी जिसे प्राकृतिक विधि-सिद्धान्तों के पुनरुत्थान (revival) का काल कहा गया है, इस सदी के प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों ने पाश्चात्य देशों की आँखें खोल दी। प्राकृतिक विधि को अब समय और स्थानानुसार परिवर्तित माना जाने लगा तथा वह वाहा एवं सापेक्ष मानी गयी। प्राकृतिक विधि की इस नई और परिवर्तित संकल्पना को ‘परिवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि’ कहा गया है। वर्तमान शताब्दी में स्टैमलर अपने द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों में कहता है कि सम्पूर्ण विध्यात्मक विधि न्यायपूर्ण विधि (होने) के लिये एक प्रयास है जो न्यायपूर्ण विधि अथवा न्याय है वह सामाजिक जीवन के ढाँचे में इच्छाओं या प्रयोजनों का एक सामंजस्य है। इच्छाओं या प्रयोजनों का सामंजस्य देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। इच्छाओं और प्रयोजनों के ज्ञान के लिये जीवन्त (living) सामाजिक संसार के यथार्थ सम्पर्क में आना होगा। वह यह निर्णय करने में समर्थ बनायेगा कि कौन प्रयोजन विधिक मान्यता के पात्र है। इस प्रक्रिया से यह पता लगाया जा सकता है कि सापेक्ष रूप से क्या न्यायपूर्ण है और यही वह ‘न्यायपूर्ण’ है जिसे प्राप्त करने का विधि को प्रयास करना चाहिये। विधि इस ‘न्यायपूर्ण’ के अनुरूप न होने पर भी मान्य है किन्तु इसे अपने लक्ष्य के निकट ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिये। इस संकल्पना को स्टैमलर ने ‘परिवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि’ कहा है।
प्रश्न 12. विधि सम्प्रभु का समादेश है। Law is the command of sovereign.
उत्तर- ऑस्टिन के अनुसार विधि सम्प्रभु का आदेश है। “Law is the command of Sovereign” ऑस्टिन के मतानुसार विधि उचित या अनुचित पर आधारित न होकर सम्प्रभु शक्ति के आदेशों पर आधारित है। अतः ऑस्टिन का निश्चित मत है कि विधि का आधार प्रभुता सम्पन्न व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में निहित है। इसी को उन्होंने आदेशात्मक सिद्धान्त (Imperative theory) कहा है।
ऑस्टिन की विधि की परिभाषा में निम्नलिखित तीन तत्व आते हैं- आदेश, सम्प्रभु और अनुशास्ति।
(1) आदेश (Command) -‘ आदेश’ राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या न करने के लिए आकांक्षा करे।
(2) सम्प्रभु (Sovereign) – ऑस्टिन ने विधि को सम्प्रभु का आदेश कहा है। ऑस्टिन ने सम्प्रभु शक्ति के दो आवश्यक लक्षण बताए हैं। प्रथम यह है कि सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जिस पर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व न हो तथा द्वितीय यह है कि सम्प्रभु शक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रजा स्वेच्छा से उसकी आज्ञा पालन के लिए इच्छुक हो।
(3) अनुशास्ति (Sanction)- ऑस्टिन ने अपने आदेशात्मक सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया है कि सम्प्रभु के आदेश मात्र ही विधि का रूप धारण नहीं करते जब तक कि उनके पीछे कोई अनुशास्ति न हो। इस प्रकार के आदेश जिनका पालन न करने पर या जिनका उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था न हो, सही अर्थ में विधि नहीं कहे जा सकते हैं।
प्रश्न 13. “समादेश” से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Command’?
उत्तर- समादेश (Command)- ऑस्टिन ने विधि को सम्प्रभु का समादेश कहा है जिसमें ‘समादेश’ राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या न करने के लिए आकांक्षा करे। आदेश सामान्य (General) या विशिष्ट (particular) दोनों प्रकार का हो सकता है। सामान्य आदेश वह है जो सभी व्यक्तियों पर सभी समयों में समान रूप से लागू रहता है, जैसे “Whoever commits murder will be hanged” जो कोई भी कत्ल करेगा, उसे फाँसी दी जायेगी। विशिष्ट आदेश वह है जो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सभी समयों के लिए अथवा सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समयों के लिए जारी किया जाय। सामान्य आदेश सकारात्मक विधि “positive law” के रूप में होता है और विशिष्ट आदेश “प्रशासी विधि” के रूप में हो सकता है।
प्रश्न 14. विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक विचारधारा में भेद कीजिए। Distinguish between Analytical and Historical School.
उत्तर- (1) विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेन्थम, ऑस्टिन, सामण्ड एवं हालैण्ड थे, जबकि ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख समर्थक सैविनी, पुत्ता, सर हेनरी मेन, हीगल थे।
(2) विश्लेषणात्मक विचारधारा के अन्तर्गत किसी भी तथ्य को विश्लेषणात्मक ढंग से ही स्वीकार किया जा सकता है तथा बिना विश्लेषण के यथावत् स्वीकार नहीं करती। इस शाखा को आज्ञात्मक शाखा भी कहा जाता है क्योंकि विधि एक समाबेश होता है जो कि एक राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया जाता है और सब के लिए समान रूप से बंधनकारी होता है। जबकि ऐतिहासिक विचारधारा में विधि के क्रमिक और स्वाभाविक विकास की ओर जोर दिया गया। इस शाखा के प्रमुख विधिशास्त्री सैविनी का कहना था कि विधि केवल अमूर्त सिद्धान्तों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है अपितु वह किसी समुदाय विशेष या देश विशेष के व्यक्तियों की आन्तरिक आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति है।
(3) विश्लेषणात्मक विचारधारा के अन्तर्गत मानव द्वारा निर्मित वास्तविक विधि को ही विधि माना गया जबकि ऐतिहासिक विचारधारा के अन्तर्गत विधि का निर्माण मानव द्वारा न होकर समाज में प्रचलित रूढ़ियों या प्रथाओं से हुआ है। इस विचारधारा के अनुसार विधि बनाई नहीं जाती, बल्कि समाज में पायी जाती है।
प्रश्न 15. विधि के विशुद्ध सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। Discuss the pure theory of Law.
Or
केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धान्त की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। Discuss the main features of Kelson’s pure theory of Law.
उत्तर- हेन्स केल्सन विधि के विशुद्ध सिद्धान्त के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। केल्सन के सिद्धान्त को “विशुद्ध विधि का सिद्धान्त” इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कानून सम्बन्धी विचारधारा के प्रतिपादन में किसी भी चीज जैसे- इतिहास, राजनीति, समाज, नैतिकता, आर्थिक तथ्यों की सहायता नहीं ली। केल्सन का विशुद्ध सिद्धान्त मानकों की एक क्रमवद्ध श्रृंखला है। उन्होंने विधिक क्रम को मानकों का स्तूप माना। उनके सिद्धान्त की आधारशिला उनका मानक है।
कैल्सन के विशुद्ध सिद्धान्त की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ नियम अन्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जाते हैं।
(2) शास्ति का विधि से परे कोई अस्तित्व नहीं है।
(3) विधि की अनुशास्ति स्वयं उसी में अन्तर्निहित होती है।
(4) पब्लिक एवं प्राइवेट विधि में अंतर नहीं है क्योंकि दोनों विधियों का एक ही स्रोत है और वह है प्रधान मानक।
(5) विधिक चाहिए मानक एवं नैतिक मानक में अन्तर है। विधिक चाहिए वाह्य जगत से जबकि नैतिक चाहिए आत्मचेतना से प्राप्त किया जाता है।
(6) समाज में शान्ति व सुरक्षा के लिए अनुशास्ति होना अपरिहार्य है।
(7) मानकों की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी मूल मानक होती है और सभी मानकों का निकास मूल मानक से होता है।
(8) मानकों की वैधता का निर्धारण मूल मानक से होता है और प्रत्येक कानूनी व्यवस्था में एक मूल मानक अवश्य होता है।
प्रश्न 16. प्राकृतिक विधि से क्या तात्पर्य है? What is meant by Natural Law?
उत्तर- प्राकृतिक विधि (Natural Law) – विधिशास्त्र में ‘प्राकृतिक विधि’ पद का तात्पर्य उन नियमों और सिद्धान्तों से है जो किसी सर्वोपरि स्रोत से निकले हुए समझे जाते हैं। प्राकृतिक विधि के नियम मनुष्य में एक स्वाभाविक गुण अच्छाई करने की होती है। इस गुण की अनुरूपता में प्राकृतिक विधि में वह सब कुछ आता है जो मानव जीवन के परिरक्षण के लिए होता है और जो इसके नष्ट होने के प्रतिकूल है। दूसरे मनुष्य में एक अन्य सहज प्रवृत्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप एक विनिर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने की होती है जो पशुओं में भी होती है। इस प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक विधि में वे सब सहज वृत्तियाँ आती हैं जिसे प्राकृतिक विधि ने सभी पशुओं पर प्रकट कर रखा है, जैसा कि नर-मादा सम्बन्ध, बच्चे उत्पन्न करना और उनका पालन करना इत्यादि बातें।
प्रश्न 17. अनुनयी निर्णय से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Persuasive Precedents?
उत्तर- अनुनयी निर्णय (Persuasive Precedents)- अनुनगी पूर्व निर्णय का अर्थ न्यायालय के एक ऐसे निर्णय से है जो दूसरे न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होते हैं परन्तु ऐसे निर्णय सम्मान के योग्य हैं। इस प्रकार एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय के लिए अनुनयी निर्णय (Persuasive Precedent) है। एक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को दूसरे राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है अतः ये निर्णय आधिकारिक (Authoritative) न होकर अनुनयी पूर्व निर्णय (Persuasive Precedent) हैं। अनुनयो पूर्व निर्णय विधि के स्रोत नहीं हैं। इसी प्रकार आंग्ल न्यायालयों तथा अमेरिकी न्यायालयों के निर्णय भारतीय उच्च या उच्चतम न्यायालय पर बाध्य नहीं हैं। ये इनके लिए अनुनयो निर्णय हैं।
प्रश्न 18. प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। Discuss main features of Natural Law School.
उत्तर- प्राकृतिक विधि के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-
(1) नियमों का स्रोत कोई सांसारिक प्राधिकारी नहीं– प्राकृतिक विधि वे नियम और सिद्धान्त हैं जो किसी सर्वोपरि स्रोत से निकले हुए समझे जाते हैं। प्राकृतिक विधि के स्त्रोत, प्रामाणिकता तथा अन्य किसी विधि के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में प्राचीन काल से ही विभित्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धान्त यद्यपि विभित्र प्रकृति के ही और परस्पर विरोधी आदर्शों का समर्थन करते हैं किन्तु इस सामान्य आधार से उद्भूत होते हैं कि इन नियमों का स्रोत कोई सांसारिक प्राधिकारी नहीं है।
(2) ये नियम बन्धनकारी होते हैं- प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त की यह पूर्वमान्यता है कि प्राकृतिक विधि के नियम बन्धनकारी होते हैं। जो कानून प्राकृतिक नियमों के खिलाफ होता है, वह बन्धनकारी स्वभाव वाला होता है।
(3) विधि तथा नैतिकता का अदभुत समन्वय- प्राचीन काल में प्राकृतिक विधि को दैवी विधि समझा जाता था। प्राकृतिक विधि व्यक्ति या समाज की प्रकृति में अन्तर्निहित होती है। यह ईश्वरीय इच्छा से निकलती है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं होती है अपितु इसका आधार नैतिकता है। प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त में हमें विधि और नैतिकता का एक अद्भुत समन्वय प्राप्त होता है।
(4) शाश्वत एवं विश्वव्यापी नियम में विश्वास- प्राकृतिक विधि में दैवी विधि का समावेश है। यह गुण-दोष, अच्छाई बुराई में विभेद करता है तथा एक आदर्श की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है। प्राकृतिक विधि सिद्धान्त एक ऐसे कानून में विश्वास करता है जिसमें शाश्वतता, जो विश्वव्यापी है तथा प्रत्येक काल व स्थान पर समान रूप से लागू होने की क्षमता रखता है।
प्रश्न 19. सामाजिक संविदा के सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए। Discuss social contract theory.
उत्तर- पुनर्जागरण काल (Renaissance) में व्यक्तिवाद को निरन्तर प्रोत्साहन मिलत रहा जिसके स्पष्ट संकेत हमें सन् 1789 की फ्रांस की क्रांति तथा अमेरिका की स्वतन्त्रता- घोषणा से मिलते हैं। एक और पुनर्जागृति के कारण समाज में नव-चेतन की लहर आई थी तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति भी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। राज्य चर्च के बन्धनों के बीच आ गया था। राज्य और जनता के बीच बढ़ते हुए विरोध को सामाजिक संविदा के सिद्धान्त (Social Contract Theory) द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया।
वैसे तो सामाजिक संविदा के सिद्धान्त का उल्लेख प्लूटो के रिपब्लिक में भी मिलता है। आदिकाल में जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो न कोई कानून था और न कोई राज्य या अन्य व्यवस्था ही थी। उस समय मानव अपनी प्राकृतिक अवस्था में था परन्तु स्वच्छन्द जीवन से ऊबकर व्यक्तियों ने आपस में शान्तिपूर्वक रहने एवं एक-दूसरे का आदर करने का समझौता किया जिसे पेक्टम यूनियनिस्ट (Pactum Unionist) कहा गया। इसी समझौते के साथ-साथ लोगों ने एक और समझौता किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने स्वयं द्वारा चुनी हुई सरकार के आदेशों का पालन करने का करार किया। इस दूसरे समझौते को पेक्टम सब्जेक्शनिक्स कहा गया। आरम्भ में सामाजिक संविदा को केवल एक ऐतिहासिक तथ्य-मात्र माना गया था। परन्तु इसके विकास के दूसरे चरण में इसे वैधानिक तर्क का आधार समझा गया।
सामाजिक संविदा के सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक ह्यूगो, ग्रोशियस, हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो थे। इन समर्थकों के विचार भित्र-भित्र थे परन्तु फिर भी प्रायः सभी विचारकों ने यह स्वीकार किया कि, ” राजनीतिक शक्ति केवल जनता में ही निहित होती है। राज्य की जन्मदायी जनता है तथा जनता के बिना राज्य का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं हो सकता।”
प्रश्न 20. ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य लक्षण। Main features of historical school.
उत्तर- ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य लक्षण या विशेषताएँ- सैविनी को ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। सैविनी ने लोक चेतना के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-
(1) इस विचारधारा के चिन्तकों द्वारा यह कहा गया कि विधि लोगों की भाषा और आचार की भाँति अपना स्वरूप ग्रहण करती है और परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होती है। यह मत व्यक्त किया गया कि विधि एक क्रमिक और काषिक प्रक्रिया से विकसित होती है। विधि लोक जीवन से उत्पन्न होती है और उसकी भावना की अभिव्यक्ति है।
(2) ऐतिहासिक विचारधारा ने एक सत्य को स्थापित किया कि किसी राष्ट्र की विधि प्रणाली पर लोगों की संस्कृति और चरित्र का बहुत प्रभाव होता है। यह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है।
(3) ऐतिहासिक विचारधारा ने अनेक परवर्ती विधिशास्त्रियों को प्रभावित किया। इस विचार में कि विधि लोोगों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है और क्रमशः विकसित होती है, भावी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के बीज निहित थे। इस विचारधारा द्वारा समाज और विधि के विकास के बीच एक कड़ी स्थापित की गई।
(4) ऐतिहासिक विचारधारा ने इतिहास में जो रुचि उत्पन्न की, उसने और आगे विधि सम्बन्धी शोध कार्यों को प्रेरणा दी। इतिहास के अध्ययन द्वारा अनेक विधिशास्त्रियों ने विधि के विकास के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और बाद में एक तुलनात्मक विधि विज्ञान की प्रणाली का आविर्भाव हुआ। इससे विधि में तुलनात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। तुलनात्मक प्रणाली से विभिन्न विधि प्रणालियों को एक दूसरे के निकट आने में सहायता मिली है। इससे प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि और लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की अनेक सम्भावनाएँ हैं।
प्रश्न 21. ‘लोक चेतना’ की व्याख्या कीजिए। Discuss the ‘Volkgist’.
उत्तर- सैविनी ऐतिहासिक पद्धति का जन्मदाता समझा जाता है। सैविनी के सिद्धान्त को सामान्य अन्तर्चेतना का सिद्धान्तं या लोक चेतना का सिद्धान्त कहते हैं। सैविनी ने अपने सिद्धान्त में कहा कि-कानून अमूर्त सिद्धान्तों और नियमों का संग्रह मात्र नहीं है अपितु वह किसी विशिष्ट मानव समुदाय या देश के व्यक्तियों की आन्तरिक आवश्यकता और उनकीं समान भावना की अभिव्यक्ति व्यक्ति है। कानून वास्तव में व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से उत्पन्न हुई चेतना की छाया है। सैविनी ने यह भी कहा कि “राष्ट्र तथा विधि में एक ऐतिहासिक सम्बन्ध है। राष्ट्र के विकास के साथ-साथ कानून (विधि) भी विकसित होता है, जब राष्ट्र में शक्ति आती है तो विधि भी शक्तिशाली हो जाती है। परन्तु जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो कानून का विनाश हो जाता है।” उन्होंने “राष्ट्र” शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ पर “राष्ट्र” शब्द का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समुदाय से है जो सामयिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक श्रृंखलाओं द्वारा एक-दूसरे से सूत्रबद्ध हैं। सारांश में सैविनी ने विधि को “जनजीवन की सामान्य लोक चेतना” कहा। इसलिए उनके विचारों को सामान्य लोक चेतना का सिद्धान्त कहा गया। सैविनी के सामान्य लोक चेतना के सिद्धान्त के आधारभूत तत्व इस प्रकार से हैं–
(1) विधि निर्मित नहीं की जाती अपितु वह जन-समुदाय में विद्यमान रहती है।
(2) विधि चेतनाहीन विकास की एक वस्तु है। सैविनी के अनुसार जिस प्रकार भाषा का विकास होता है, उसी प्रकार विधि का भी विकास होता है।
(3) विधायन सामान्यतः चेतना के अनुसार होना चाहिए। विधि सदैव प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख होती है। विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन होने के साथ समाप्त होती है और यही इसकी विशेषता है।
(4) कानून का स्वभाव सार्वभौमिक नहीं होता है और न ही इसे सभी स्थानों पर समान रूप से लागू ही किया जा सकता है। विधि देश-विदेश के अनुसार वहाँ के लोगों की भावनाओं और धारणाओं के अनुकूल बदलती रहती है। किसी देश की विधि ही वहाँ के जनसमुदाय की लोक चेतना है। प्रश्न
22. विधिशास्त्र में ऐतिहासिक विचारधारा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate the contribution of historical school in Jurisprudence.
उत्तर- विधिशास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों ने विधि के विकास के लिए उसके ऐतिहासिक क्रमिक विकास के अध्ययन को आवश्यक माना है। विधि की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को विकसित करन का वास्तविक श्रेय ऐतिहासिक विधिशास्त्रियों को ही है जिसके परिणामस्वरूप विधि के चिन्तन को एक नई दिशा मिली। ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थकों का तर्कहै कि विधि बनाई जाने के बजाय उसे अतीत से खोजा जाना चाहिए क्योंकि उसका स्वअस्तित्व होता है। वे प्रथा को विधि का औपचारिक स्रोत मानते हुए उसके बन्धनकारी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। इन विधिशास्त्रियों का मत है कि विधान तथा न्यायिक पूर्वोक्तियाँ प्रथाओं को बल नहीं देतीं।
प्रश्न 23. वास्तविक (यथार्थवादी) विचारधारा से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Realist Theory’ of Law?
उत्तर- वास्तविक विचारधारा (Realist Theory)- इसे यथार्थवादी विचारधारा भी कहा जाता है। विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा, विधि के उन पहलुओं पर ध्यान देती हैं जो विधि को न्यायालय द्वारा लागू करने से सम्बन्धित हैं। विधि इन यथार्थवादियों के अनुसार न्यायाधीशों से निकलती है। इस विचारधारा के अनुसार विधि वह नहीं है जो विधि पुस्तकों में अन्तर्निहित है अपितु विधि वह है जो न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से लागू की जाती है। न्यायमूर्ति ओलिवर वेण्डेल होम्स (1841-1936) विधि की यथार्थवादी विचारधारा के आन्दोलन के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। विधि की यथार्थवादी विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्रियों में न्यायमूर्ति ओलिवर वेण्डेल होम्स (Oliver Vendell Homes) एक प्रमुख विधिशास्त्री हैं। न्यायमूर्ति होम्स ने बोस्टन विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए विचार व्यक्त किया कि “न्यायालय में न्यायाधीश जो उद्घोषणाएं करते हैं, मेरे विचार में विधि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।”
यथार्थवादी विचारधारा का यह सिद्धान्त हो गया है कि विधि का शासन आचरण की विधि है। जब विधि की अधिकारिता को चुनौती दी जाती है, निर्णय करते समय जो घोषणाएँ न्यायालय द्वारा विधि की निश्चिततापूर्वक व्याख्या की जाती है तथा जिसे न्यायालय उचित मानते हैं, इसके अतिरिक्त विधि कुछ नहीं है।
प्रश्न 24. अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए? Write a short note on American Realist School.
उत्तर- अमेरिकी यथार्थवाद सामाजिक संस्थाओं के प्रति फलवादी (pragmatist) और व्यवहारवादी (behaviourist) दृष्टिकोण की उपज है। वकीलों ने इसका विकास विश्लेषणात्मक विध्यात्मवाद (analytical pisitivism) के दर्शन, जो उन्नीसवीं शताब्दी में आंग्ल-अमेरिकी विधिशास्त्र पर छाया हुआ था, को सुधारने के रूप में न्यायालयों के कार्य और न्यायिक व्यवहार पर जोर देते हुए किया है। उन्होंने विधिक संकल्पनावाद (legal conceptionalism) के विपरीत कार्यशील विधि और अनुभव के रूप में विधि पर बल दिया है तथापि, उन्होंने विधि के सर्वव्यापक आधार से सरोकार नहीं रखा है जबकि वे विधि के साक्षेपवादी दर्शन (relativistic philosophy of law) से सहमत होने को उन्मुख हुए हैं। किन्तु श्री फैकिल्स कोहन को छोड़कर, अमेरिकी यथार्थवादियों ने मूल्यों के किसी दर्शन को कथित करने का प्रयत्न नहीं किया है। लेबेलिन के शब्दों में अध्ययन के प्रयोजन के लिए वे ‘क्या’ है और ‘क्या होना चाहिए’ के बीच एक अस्थायी अलगाव मानकर चले हैं।
न्यायशास्त्रीय आधारों की दृष्टि से अमेरिकी यथार्थवाद महाद्वीपीय आन्दोलन का समरूप है और एहरलिच इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। इनके बीच लक्षणगत (characteristic) अन्तर, न्यायालयों के विनिश्चयों पर भिन्न-भिन्न रूप से दिये गये जोर पर है। तभी आंग्ल अमेरिकी वकीलों के समान अमेरिकी यथार्थवादी न्यायालयों के विनिश्चय को विधि का केन्द्र बनाने को तत्पर होते हैं और वस्तुतः विधि की परिभाषा को न्यायालयों के विनिश्चयों पर केन्द्रित करते हैं जबकि एहरलिच अपना मुख्य ध्यान उस पर देते हैं जिसे वह सजीव विधि (living law) कहते हैं, अर्थात् आचरण के नियमों और आदतों की संहिता जिनमें से अधिकांश कभी भी न्यायालयों के समक्ष आते ही नहीं। इन दो प्रणालियों (systems) के अन्तर्गत वकीलों की ऐतिहासिक और प्रणालीबद्ध पृष्ठभूमि ही दृष्टिकोण के इस अन्तर में अपनी भूमिका अदा करती है।
प्रश्न 25. आर्थिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं?What do you understand by Economical School?
उत्तर- अर्थशास्त्रीय विचारधारा (Economical School) – अर्थशास्त्रीय विचारधारा वास्तव में समाजशास्त्रीय विचारधारा का एक परिमार्जित रूप है जो विधि के स्वरूप और महत्व का निर्धारण आर्थिक दृष्टिकोण से करती है। इस पद्धति का प्रमुख सिद्धान्त यह है कि सांविधिक नियमों की व्याख्या और उसका अर्थान्वयन कार्ल मार्क्स और ऐंजिल्स के द्वारा व्यक्त किये गये सामाजिक और राजनीतिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स और ऐंजिल्स ने विधिक विचारधारा के सम्बन्ध मे बहुत कम लिखा है। मार्क्स का मत है कि “वर्ग” प्रधान है तथा “राज्य” और “विधि” गौण है। राज्य तो “वर्ग” की इच्छा को कार्यान्वित करने का माध्यम है और “विधि” उसको कार्यान्वित करने का एक अस्त्र है।
प्रश्न 26. बेन्थम की उपयोगितावादी विचारधारा?Bentham’s theory of utilisation.
उत्तर- बेन्थम का उपयोगितावादी सिद्धान्त – उपयोगितावाद आचारशास्त्र का एक सिद्धान्त या नीति है जिसमें यह बताया गया है कि जो कुछ उपयोगी है। वही श्रेष्ठ है अतः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धान्तों तथा नीतियों को उपयोगितावाद के सिद्धान्त के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। उपयोगितावाद मानव जाति के कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है जो युक्तिसंगत तर्कों के आधार पर मानव जाति की दशा को सुधारने तथा प्रभावशाली राज्य विधायन के द्वारा जनता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए वास्तविक प्रयासों को सर्वाधिक महत्व देता है। इसका मूल उद्देश्य लोक कल्याण को प्रमुखता देना है। बेन्थम तथा उसके अनुयायी जेम्स मिल तथा जॉन स्टुअर्ट मिल (पिता-पुत्र) ने उपयोगितावादी सिद्धान्त को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया। अतः यह सिद्धान्त नैतिक एवं राजनैतिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। नैतिक सिद्धान्त के रूप में इसे “सार्वभौमिक सुखवाद” कहा जा सकता है। यह सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य मुख्य रूप से एक इन्द्रिय प्रधान प्राणी है जो सदैव सुख की कामना रखता है तथा दुःख से बचना चाहता है। प्रत्येक वह कार्य जो दुःख की अपेक्षा अधिक सुख है, अच्छा या सही है। इस प्रकार सुख समस्त मानव प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है। अतः उपयोगितावाद का प्रथम तथा अन्तिम उद्देश्य जीवन, मानव-कर्म तथा मानव कल्याण द्वारा सुख की समृद्धि करना है तथा राजनीतिक दृष्टि से इसे अन्याय एवं अत्याचार विरोधी कहा जा सकता है। यह स्वाभाविकतः ही मानव की वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सर्वाधिक महत्व देता है जो राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप द्वारा ही सम्भव है। उपयोगितावाद का ध्येय केवल ‘रोटी कपड़ा मकान’ तक ही सीमित न होकर इसके द्वारा मानव की बौद्धिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, नैतिक एवं सामाजिक विचारों को परिष्कृत करने का प्रयास भी किया जाता है।
प्रश्न 27. सामाजिक स्वामित्व से क्या तात्पर्य है? What is meant by social ownership?
उत्तर- सामाजिक स्वामित्व – ऐतिहासिक रूप से पहले कथा की संकल्पना अस्तित्व में आई और उसके बाद समाज के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तनों के कारण स्वामित्व की संकल्पना विकसित हुई। स्वामित्व की संकल्पना उस वक्त अस्तित्व में आई प्रतीत होती है जबकि समाज खानाबदोशी से कृषि प्रधान समाज में परिवर्तित हुआ विकास का यह क्रम इस सिद्धान्त को स्पष्ट करता है कि विधि और समाज का विकास परस्पर सम्बन्धित है और इसलिये एक को दूसरे के बिना पूर्णतः समझा नहीं जा सकता।
स्वामित्व की परिभाषा ऑस्टिन के अनुसार, “स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बन्धित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है।” हॉलैण्ड ने भी इसी परिभाषा को अपनाया है। उनके अनुसार, “किसी वस्तु पर पूर्ण नियन्त्रण ही स्वामित्व है।” सामण्ड महोदय ऑस्टिन की परिभाषा से सहमत नहीं हैं। सामण्ड कहते हैं कि “स्वामित्व व्यापक रूप में व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को किसी वस्तु पर प्राप्त अधिकार के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है।” इसके अनुसार स्वामित्व में सभी प्रकार के अधिकार सम्मिलित होते हैं चाहे वे साम्पत्तिक हों या व्यक्तिगत, स्वासाम्पत्तिक हों या परसाम्पत्तिक, चाहे वे सार्वभौमिक हों या व्यक्तिलक्षी।
प्रश्न 28. जैसा समाज होगा वैसी ही विधि होगी- समझाइए।As is society so is the Law (UBI SOCIETA IBI LEX). illustrate.
उत्तर- जहाँ समाज है वहीं विधि है (Where there is society, there is law) 1 यह विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा का यन्त्र वाक्य है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री कहते हैं कि विधि समाज में भाषा की भाँति विकसित होती है। अतः जैसा समाज होगा, वैसी ही विधि होगी। विधि समाज के अनुरूप होनी चाहिए। प्रगतिशील समाज में प्रगतिशील विधि होगी तथा जंगली समाज में विधि अन्य मान्यताओं पर आधारित होगी। हिन्दू विधि तथा मुस्लिम विधि या भारत की पारिवारिक विधि इस सूत्र वाक्य का उदाहरण है। भिन्न-भिन्न समाज में भिन्न-भिन्न प्रथाएं होती हैं। यही प्रथाएँ वास्तव में विधि का स्रोत हैं। इस प्रकार समाज के अनुरूप विधि का होना ऐतिहासिक विचारधारा का यन्त्र वाक्य है। जनजातीय कवियों में उनके समाज के अनुरूप नियम तथा परिनियम बने हैं। भारत में भी सामान्य दीवानी संहिता (Common Civil Code) की परिकल्पना भी सामाजिक विभिन्नता के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में भी हम विभिन्न प्रकार की विधियों का अस्तित्व पाते हैं। आज समलैंगिक सम्बन्ध को कुछ यूरोपीय देशों में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यह उनके समाज के अनुरूप हो सकती है परन्तु हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में ही विभिन्न प्रदेशों की विधायिकाओं ने अपने समाज के अनुरूप विधियों का अधिनियमन किया है। अतः यह कहना सही होगा कि जैसा समाज होगा वैसा ही विधि होगी (UBI SOCIETA IBI LEX)।
प्रश्न 29. ‘सामाजिक समेकता’ के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।Discuss the doctrine of ‘Social Solidarity’.
उत्तर- सामाजिक समेकता (Social Solidarity) मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। वह अपने साथियों के साथ जीवन व्यतीत करता है तथा ऐसा करते समय उसे अपने साथियों से मिलना होगा। ऐसा करते समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए तथा हितों की पूर्ति के लिए समाज में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यही परस्पर निर्भरता का सिद्धान्त (Doctrine of Interdependence) ड्यूगिट के विधि एवं समाज सम्बन्धी विचार का मूल बिन्दु है। यह परस्पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे समाज विषम (Complex) होता है, लोगों की अपनी समान आवश्यकता होती है जो अपनी पूर्ति के लिए संप्रभु प्रयास करना चाहती है। समाज के सदस्यों की आवश्यताएं भिन्न-भिन्न होती हैं। ये भिन्न आवश्यकताएं समाज के लोगों में समायोजन (Adjustment) तथा मेल-मिलाप की अपेक्षा करती हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सहयोग तथा सेवाओं की अपेक्षा करता है तथा इसे प्राप्त करता है। आज समाज का कोई भी सदस्य दूसरे व्यक्ति की सेवा तथा सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता। सामाजिक परस्पर निर्भरता (Social mutual Interdependance) मानव अस्तित्व का अपरिहार्य तथ्य है। समाज के सभी सदस्यों को परस्पर पूर्ण सहयोग तथा समेकता (Solidarity) लाने का प्रयास करना चाहिए। इसे सामाजिक समेकता (Social Solidarity) कहते हैं। ड्यूगिट के अनुसार विधि का सामाजिक कार्य सामाजिक समेकता, समाजिक एकता (Social Solidarity) प्राप्त करना है।
प्रश्न 30. विधि के संहिताकरण पर सैविनी का क्या विचार था? स्पष्ट करें। What was Savigny’s opinion on codification of Law? Explain.
उत्तर- ऐतिहासिक विचारधारा के जनक सैविनी का निश्चित मत था कि विधि स्थायी स्वरूप की नहीं होती है तथा वह जनभावना के अनुरूप सदैव परिवर्तित होती रहती है। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की विधि उस राष्ट्र के विकास के साथ विकसित होती रहती है, बढ़ती रहती है तथा उस राष्ट्र के विघटन के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए सैविनी जर्मन विधि के संहिताकरण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे विधि के विकास की गति रुक जाने की ठीक उसी प्रकार सम्भावना थी जिस प्रकार कि किसी अवरुद्ध तालाब का पानी निकासी के अभाव में रुका रह जाता है।
उनके द्वारा जर्मन विधि के संहिताकरण का विरोध किये जाने का एक अन्य कारण यह भी था कि उस समय जर्मनी में लोक चेतना (Volkgeist) का पर्याप्त विकास न हुआ होने के कारण संहिताकरण से विधि का विकास अवरुद्ध हो जाने की सम्भावना थी।
प्रश्न 31. सर हेनरी मेन के स्थिर समाज एवं प्रगतिशील समाज के चरण को स्पष्ट करें। Explain Sir Henry Maine’s stages of static society and progressive society.
उत्तर- आंग्ल विधि के ऐतिहासिक विकास में सर हेनरी मेन का नाम उल्लेखनीय है, “न्होंने जर्मन ऐतिहासिक पद्धति के अन्तर्गत प्रकाशित रोमन विधि और उसके विकास का सर्वांगीण अध्ययन किया। वे इंग्लिश, रोमन तथा हिन्दू विधि के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने विभिन्न देशों की विधि-प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करके विधि के विकास सम्बन्धी कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले। हिन्दू विधि तथा रोमन विधि के तुलनात्मक अध्ययन के बाद उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि समाज या तो स्थिर (Static) होता है अथवा विकासशील (Progressive)। इन दोनों प्रकार के समाजों के विधिक विकास में भिन्नता होती है तथापि मेन का यह निश्चित मत था कि ये दोनों प्रकार के समाज अपनी प्रारम्भिक अवस्था में निम्नलिखित विधिक चरणों में से गुजरते हैं-
(1) प्रथम चरण में विधि का विकास वैयक्तिक आदेश द्वारा प्रारम्भ होता है। इस अवस्था में शासक के वैयक्तिक आदेशों को ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक माना जाता है।
(2) द्वितीय चरण में उपर्युक्त आदेश प्रथा का स्वरूप ले लेता है।
(3) तृतीय चरण में शासक के स्थान पर कुछ सीमित लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, जो स्वयं विधियों को प्रसारित करते हैं।
(4) चतुर्थ चरण में बहुजन समुदाय विधि-निर्माताओं के विरुद्ध विद्रोह करते हैं जिसके परिणामस्वरूप विधि प्रसारित होकर संहिता का रूप धारण कर लेती है।
उपर्युक्त चार अवस्थाओं तक स्थिर तथा विकासशील, इन दोनों ही प्रकार के समाज में विधियों का विकास एक समान होता है। परन्तु चतुर्थ चरण में पहुँचने के पश्चात् स्थिर समाज आगे विकसित नहीं हो पाता है। अतः उसकी विधियों का विकास भी कुंठित हो जाता है किन्तु विकासशील समाज में विधि का विकास वैधानिक परिकल्पनाओं (Legal Fictions), साम्या (Euity) तथा विधायन (Legislation) के माध्यम से निरन्तर जारी रहता है।
प्रश्न 32. सैविनी एवं मेन के विवारों की भिन्नता पर प्रकाश डालिए। Elucidate the differences between the thoughts of Savigny and Maine.
उत्तर- सैविनी और नरी मेन की विचारधारा में अन्तर- यद्यपि सैविनी तथा सर हेनरी मेन दोनों ही विधिशास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक थे परन्तु अनेक बातों में उनके विचार एक-दूसरे से भिन्न हैं। जहाँ एक ओर सैविनी ने प्रथाओं को महत्व दिया वहीं दूसरी ओर हेनरी मेन ने सभ्यता के विकास के साथ विधायन द्वारा निर्मित संहिताबद्ध विधि की आवश्यकता पर बल दिया। अपने तर्क की पुष्टि में हेनरी मेन ने इंग्लैण्ड की तत्कालीन विधि की अस्पष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसका मूल कारण यह था कि यह विधि प्रधान रूप से न्यायाधीशों द्वारा निर्मित की गई थी न कि विधान-मण्डल द्वारा।
हेनरी मेन ने सैविनी के ‘लोक चेतना के सिद्धान्त’ (Volkgist) को मान्य नहीं किया। उन्होंने विधान-मण्डल की सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार किया जिसे सैविनी ने मानने से इन्कार कर दिया था। वस्तुतः हेनरी मेन ने प्रगतिशील समाज के लिए विधान को विधि के निर्माण का एक अनिवार्य साधन माना है। उनका “प्रास्थिति से संविदा की ओर” (Status to Contract) का सिद्धान्त व्यावहारिक होने के साथ-साथ तत्कालीन पूँजीवादी और औद्योगिक समाज की परिस्थितियों के लिए उसी प्रकार अनुकूल था जिस प्रकार कि सैविनी का लोक चेतना का सिद्धान्त तत्कालीन जर्मन समाज की आन्तरिक भावनाओं के अनुकूल था।
प्रश्न 33. समाज की गतिविधियों का संचालन ‘संविदा से प्रास्थिति की ओर है’ इस प्रत्यय को समझाइए।
What do you understand by movement of Society from Contract to Status?
उत्तर- संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति तथा अन्य प्रगतिशील समाज में महिलाओं तथा परिवार के सदस्यों की प्रास्थिति में परिवर्तन से हेनरी मेन का यह कथन सत्य साबित हुआ कि आधुनिक समाज का संचलन प्रास्थिति (Status) से संविदा की ओर हुआ है।
परन्तु समाज की प्रगति ने अब व्यक्ति को अकेला कर दिया है। परिवार से पृथक् होकर परिवार के सदस्य की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो गई। अब व्यक्तिगत संविदा करने की कमजोरी ने सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) की आवश्यकता को जन्म दिया। व्यक्तिगत सौदेबाजी का स्थान सामूहिक सौदेबाजी ने लिया है, अब व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित प्रतिस्थापित हुआ (Individual interest was substituted by collective interest) व्यक्ति की असीमित स्वतन्त्रता ने एक नवीन दासता को जन्म दिया। यहाँ तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति की संविदा करने की क्षमता शक्तिशाली औद्योगिक जगत के समक्ष अपने को असहाय महसूस करने लगा। एक श्रमिक की व्यक्तिगत संविदात्मक क्षमता मिल मालिक की संविदात्मक क्षमता के समक्ष असहाय हो गई। अब एक नवीन प्रकार की दासता ने जन्म लिया। इसका आधार विधिक अक्षमता न होकर आर्थिक असहायता थी। अब यह आवश्यक हो गया कि व्यक्तिगत संविदा के स्थान पर सामूहिक संविदा स्थापित हो। औद्योगिक विश्व में व्यवसाय संघ (Trade Union) अपरिहार्य हो गया। अब संगठित संविदा आवश्यक हो गई। राज्य में भी व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित प्रतिस्थापित हुआ। अब एक श्रमिक की व्यक्तिगत प्रास्थिति (Status) समाप्त होने लगी। अब एक श्रमिक, श्रमिक वर्ग की इकाई के रूप में अपना अस्तित्व रखता है। भारत में भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर राज्य का नियन्त्रण बढ़ा। लोकहित पर व्यक्तिगत हित प्रभावी हुआ। लोकहित में व्यक्तिगत हित नियन्त्रित होने लगा।
अब आधुनिक समाज में सर हेनरी मेन की प्रास्थिति से संविदा की ओर समाज के संचलन की परिकल्पना ध्वस्त हो गई। इसका स्थान संविदा से प्रास्थिति की परिकल्पना ने लिया। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के स्थान पर सामूहिक स्वतन्त्रता प्रतिस्थापित हुई। संक्षेप में कहें तो आर्थिक कारकों, मानव गतिविधि पर सरकारी नियन्त्रण तथा कमजोर वर्ग के संरक्षण की नैतिक आवश्यकता ने एक नवीन प्रास्थिति को जन्म दिया। अब समाज का संचलन (Movement) संविदा से प्रास्थिति (Contract to status) की ओर हुआ और यही समाज की वर्तमान आवश्यकता तथा अपरिहार्यता है।
प्रश्न 34. रास्को पाउण्ड ने हितों का वर्गीकरण कैसे किया है?How the interest has been classified by Rosoco Pound?
उत्तर- रास्को पाउण्ड ने हितों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है-
हित (Interest)
– निजी हित (Private Interest)
– व्यक्ति सम्बन्धी हित (Interest Relating to person)
– घरेलू हित (Domestic Interest)
– धन सम्बन्धी हित (Monetary Interest)
लोक हित या राज्य हित (Public Interest)
– राज्य हित व्यक्ति के हित के संरक्षक के रूप में
– राज्य का हित (Interest of State)
– सामाजिक हित के संरक्षक के रूप में राज्य का हित
सामाजिक हित (Social Interest)
– सामाजिक हित
– सामाजिक संस्था का हित
– सामाजिक संसाधन का हित
– सामान्य नैतिकता सम्बन्धी
– सामान्य प्रगति का हित
-आर्थिक प्रगति
– राजनैतिक प्रगति
– सांस्कृतिक प्रगति
प्रश्न 35. पाउण्ड के सामाजिक हितों की समीक्षा कीजिए।Discuss the social interests of Pound.
उत्तर-पाउण्ड का सामाजिक हित (Social Interest of Pound)- पाउण्ड हितों को तीन शीर्षकों में वर्गीकृत करता है- प्राइवेट हित, लोक हित तथा सामाजिक हित। सामाजिक हित जो विधिक संरक्षा के योग्य हैं, वे हैं- (i) शान्ति और व्यवस्था के संरक्षण और सामान्य सुरक्षा के रख-रखाव में हित (ii) विवाह और धार्मिक संस्थाओं जैसी सामाजिक संस्थाओं के संरक्षण में हित (iii) भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करने, जुआ खेलने को प्रोत्साहित करने और प्रचलित नैतिकता के प्रतिकूल संव्यवहारों के अविधिमान्यकरण द्वारा सामान्य नैतिकता के संरक्षण में हित, (घ) सामाजिक साधनों के परिरक्षण में हित, (ङ) सामान्य उन्नति में हित जो शिक्षा की स्वतन्त्रता, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, व्यापार और वाणिज्य की स्वतन्त्रता द्वारा प्राप्त किया जाना और (च) मानक व्यक्तियों में हित। वह उन प्रवृत्तियों का भी पता लगाता है जिन्होंने इन हितों की संरक्षा के लिए कार्य किया।
मुख्य और अधिक आवश्यक समस्या उस रीति की है जिसके द्वारा विधिज्ञ ऐसे हितों के संतुलन और मूल्यांकन पर पहुँच सकता है। न्यायाधीश कार्डोजो ने इसकी बाबत समस्याओं को बताने का प्रयत्न किया है। उसने दाँव पर लगे सामाजिक मूल्यों और हितों के बारे में न्यायिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया है, किन्तु वह न्यायाधीश की स्वतंत्रता को अपेक्षाकृत बँधे हुए, यद्यपि महत्वपूर्ण क्षेत्र तक, सौमित रखता है जो तब रहती है जब विधि को पाने के अधिक निश्चित स्रोत समाप्त हो गए हैं। उसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं –
“तर्क और इतिहास, रूढ़ि और उपयोगिता और ठीक आचरण के स्वीकृत मानक वे शक्तियाँ हैं जो अकेले या मिलकर विधि के विकास को रूप देते हैं। इनमें से कौन शक्ति किस मामले में हावी होती है यह एक बड़े रूप में अपेक्षाकृत उन सामाजिक हितों के मूल्य के किस महत्व पर निर्भर करेगा जो उसके द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे अथवा बिगाड़े जाएंगे। एक सबसे बड़ा मूलभूत सामाजिक हित यह है कि विधि एक रूप और निष्पक्ष होगी। उसके काम करने में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे पूर्वाग्रह अथवा पक्षपात अथवा मनमानी अथवा मनमौज झलके। इसलिए प्रधानरूप से पूर्व निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। इतिहास अथवा रूढ़ि का संगत रूप से समरूप चालक शक्ति रही हो और तर्क अथवा दर्शन में समरूपता तब होगी जब चालक शक्ति वे होंगे। किन्तु समरूप विकास एक बड़ी कीमत पर लाया जा सकता है। एकरूपता उस समय भलाई नहीं रह जाती जब वह सताने की एकरूपता हो जाती है। समरूपता अथवा निश्चितता से प्राप्त होने वाला साम्य, ऋजुता अथवा सामाजिक कल्याण के अन्य तत्वों द्वारा पहुँचाये जाने वाले सामाजिक हित के साथ संतुलित होना चाहिए। ये न्यायाधीश पर यह कर्तव्य डालते हैं कि वह एक दूसरे कोण पर रेखा खींचे, नई दिशा में मार्ग बनाये, हटकर चलने की एक नई बात लायें जिससे उसके बाद आने वाले वहाँ से अपनी यात्रा पर निकले।
प्रश्न 36. विधि का कार्य सामाजिक अभियन्त्रण है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।
“The Function of Law is social engineering”. Explain this Statement.
उत्तर- रास्को पाउण्ड विधि के कार्य को “सामाजिक यांत्रिकी” (Social Engineer- ing) बताते हैं। उनके अनुसार, विधि का कार्य सभ्यता को कायम रखना तथा उसको आगे बढ़ाना है। प्रकृति से निरन्तर संघर्ष करते हुए मनुष्य अपनी शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहे, इसी का नाम सभ्यता है। अतः कानून एक हथियार के समान है। इसका काम किसी विशेष समय में किसी विशेष सभ्यता को कायम रखना तथा उसको आगे बढ़ाना है। अतः हमारे कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
(i) खोज।
(ii) न्यायिक अभिधारणाएँ (Jural Postulates) ।
(iii) हितों की सूची तैयार करना जिन्हें कानून द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए।
(iv) विरोधी हितों में उचित मेल स्थापित करना।
प्रश्न 37. रूढ़ि से क्या तात्पर्य है? What do you mean by custom?
उत्तर- रूढ़ि (Custom) – प्राचीन समाज में शासक विधि-निर्माण का कार्य नहीं करता था। उसका न्याय जनसाधारण की उचित अनुचित की धारणाओं पर निर्भर रहता था।उचित-अनुचित का विचार लोगों के व्यवहार या रूढ़ियों में ही निहित था। समाज के लोग परिस्थिति विशेष में एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। यही व्यावहारिक अभ्यस्तता कालान्तर में रूढ़ि या प्रथा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है।
प्रथा लोगों द्वारा पालन की जाने वाली एक चलन (usage) है। यह एक ऐसा आचरण है जिसका पालन समाज के लोग स्वभावतः और आदतन करते हैं। प्रथा की निरन्तरता बनी रहती है। एक लम्बे समय तक व्यवहार में अस्तित्व रखने वाला चलन प्रथा में बदल जाता है। जब वह बाध्यकारी स्वभाव ग्रहण कर लेता है तब वह विधि का बल प्राप्त कर लेता है।
प्रश्न 38 विधि के अनुसार ‘न्याय’ से क्या तात्पर्य है? Explain what is meant by ‘Justice’ according to law?
उत्तर- यह सर्वविदित है कि विधि का मुख्य उद्देश्य मानवीय आचरणों को नियन्त्रित रखते हुए समाज में न्याय स्थापित करना है। अतः विधि और न्याय में निकटतम सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है। विधि द्वारा समाज में न्याय प्रस्थापित किया जाता है, अतः ‘न्याय’ ही विधि की मुख्य विषय-वस्तु है। ‘न्याय’ अथवा ‘न्यास प्रशासन’ की परिभाषा देते हुए सामण्ड ने कहा है कि राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा अधिकारों तथा न्याय का संरक्षण किया जाना ही ‘न्याय’ अथवा न्याय प्रशासन कहलाता है। विधि और न्याय के परस्पर सम्बन्धों के महत्व के विषय में प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल (Pascal) लिखते हैं कि शक्ति (विधि) निरंकुश होती है। विधि-विहीन न्याय एक कपोल कल्पना मात्र है क्योंकि समाज में अवांछनीय व्यक्तियों पर उचित नियन्त्रण रखने के लिए शक्ति आवश्यक है। इसी प्रकार न्याय के बिना विधि स्वयं अपूर्ण मानी जाती है। अतः न्याय और विधि को एक साथ रखा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त तर्क से पास्कल का आशय यह है कि विधि के बिना न्याय सम्भव नहीं है। इसी प्रकार बिना न्याय के विधि की कल्पना करना व्यर्थ है। अनेक विद्वान न्याय को इतना अधिक महत्व देते हैं कि वे उसे विधि का आदर्श मानते हैं। केल्सन न्याय को ही ‘सामाजिक प्रसन्नता’ कहते हैं। सिसरो महोदय के अनुसार, “विधि का पालन ही न्याय है। विधि को लागू करने वाली संस्थाएँ न्यायालय कहलाती हैं और विधि को लागू करने वाले व्यक्ति न्यायाधीश कहलाते हैं।” विनोग्रेडॉफ के अनुसार, “विधि का उद्देश्य न्याय और औचित्य की स्थापना करना है। न्याय की स्थापना से अभिप्राय यह है कि विधि का प्रवर्तन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित उपयोग कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि “विधि न्याय प्राप्त करने का साधन है।”
प्रश्न 39. दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त के गुणों पर प्रकाश डालिए। Throw light on the merits of reformative theory of punishment.
उत्तर – सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative Theory) का उद्देश्य अपराधी में सुधार लाना होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी व्यक्ति अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण अपराध करता है। अतः अपराध करने की प्रवृत्ति को अपराधी के चरित्र निर्माण द्वारा रोका जा सकता है।
सुधारात्मक सिद्धान्त के निम्नलिखित गुण हैं जो इस प्रकार हैं-
(1) सुधारात्मक सिद्धान्त अपराधी को कारागार की कोठरियों में बन्द करके यातनाएँ देना उचित नहीं समझता है अपित यह अपराधी की अपराध प्रवृत्तियों का उपचार करके उसे सदा के लिए सुधार देना ही उचित समझता है।
(2) सुधारात्मक सिद्धान्त में अपराधी को दोषी या अपराधी न मानकर एक बीमार व्यक्ति माना जाये और उसकी चिकित्सा की जाये। उसने अपराध क्यों किया? इसका अध्ययन पारिवारिक, मानसिक, शैक्षिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किया जाये और ऐसा नैतिक वातावरण बनाया जाये जिससे कि वह अपने आपको सुधार सके।
प्रश्न 40. रूढ़ि तथा विरभोगाधिकार में अन्तर स्पष्ट करें। Differentiate between custom and prescription.
उत्तर- रूढ़ि तथा चिरभोगाधिकार में अन्तर (Difference between Custom and Prescription)- ऐतिहासिक दृष्टि से चिरभोगाधिकार रूढ़िजन्य विधि का ही एक प्रकार मात्र है। प्रारम्भ में चिरभोगाधिकार को व्यक्तिगत रूढ़ि माना जाता था। इस अर्थ में यह किसी विशिष्ट व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों या पूर्वोपभोगियों के अधिकारों तक सीमित था। तथापि रूढ़ि और चिरभोगाधिकार में निम्नलिखित अन्तर हैं-
(1) चिरभोगाधिकार व्यक्तिगत स्वरूप का होता है तथा वह विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति लागू होता है जबकि स्थानीय रूढ़ि का सम्बन्ध स्थान-विशेष से है न कि व्यक्ति-विशेष से।
(2) विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ि को प्रभावशाली दीर्घकालीन व्यवहार या आचरण माना गया है जबकि चिरभोगाधिकार को केवल अधिकार के स्रोत के रूप में दीर्घकालीन आचरण माना गया है।
(3) विधिक मान्यता के लिए रूढ़ि का अस्तित्व चिरकालीन होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी विनिर्दिष्ट न्यूनतम अवधि तक किया गया हो। उदाहरण के लिए किसी भवन के सम्बन्ध में हवा या प्रकाश का उपयोग बीस वर्ष तक निरन्तर किये जाने पर चिरभोगाधिकार प्राप्त हो सकता है।
(4) रूढ़ि की वैधता के लिए वह न्याय तथा लोकोपयोगिता के अनुरूप होनी आवश्यक है, किन्तु चिरभोगाधिकार के लिए यह आवश्यक है।
(5) रूढ़ि दीर्घकालीन प्रथा पर आधारित है जबकि चिरभोगाधिकार का उद्भव किसी अधिकार के त्यजन के परिणामस्वरूप होता है।
प्रश्न 41. सर्वोच्च विधायन को स्पष्ट करें। Explain Supreme Legislation.
उत्तर – सर्वोच्च विधायन (Supreme Legislation) – सर्वोच्च विधायन वह विधायन है जिसका उद्भव राज्य की सम्प्रभु शक्ति (Sovereign Power) से होता है और जो किसी भी बाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र होता है। यह सर्वोच्च इसलिए कहा जाता है कि राज्य में कोई ऐसी दूसरी शक्ति नहीं हुआ करती जो इसकी सार्वभौमिकता को चुनौती दे सके, उसे काट सके या बदल सके।
इस प्रकार सर्वोच्च विधायन वह होता है जो विधायिनी शक्ति रखने वाली संस्था या निकाय से पारित किया गया हो जो सर्वोच्च स्थान रखती है। उसका विधान सबके लिए बन्धनकारी होता है तथा उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। जैसे- इंग्लैण्ड में संसद का विधायन सर्वोच्च होता है।
सर्वोच्च विधायन के सन्दर्भ में भारतीय संसद की स्थिति वैसी नहीं है जैसी इंग्लैण्ड की संसद की है क्योंकि भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सर्वोच्च विधायन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि भारत की संसद पूर्णतः प्रभुतासम्पन्न होते हुए भी उनके द्वारा अधिनियमित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में संसद या राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये कानून की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वे संविधान सम्मत नहीं हैं।
इन्दिरा गाँधी बनाम राजनारायण, ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 2293 सम्बन्धी मामला उक्त कथनों पर आधारित है।
इस प्रकार भारतीय संसद सम्प्रभु है परन्तु उसमें वैधानिक नियन्त्रण लगा दिया गया है। भारत में संविधान होने के कारण कोई भी विधान पहले इस कसौटी पर कसा जाता है कि वह संविधान सम्मत है या नहीं। इसीलिए भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान नहीं है।
प्रश्न 42 प्रत्यायोजित विधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।Write short notes on delegated legislation.
उत्तर – प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)- एक प्रकार का अधीनस्थ विधान (Subordinate Legislation) है। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है-उच्च विधायी सत्ता द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कार्यपालिका द्वारा बनायी गयी विधि कभी-कभी कानून बनाने वाली संस्था व्यापक व्यस्तता के कारण जब किसी विषय पर कानून निर्माण का कार्य किसी अधीनस्थ संस्था को सौंप देती है तो ऐसी स्थिति में उस अधीनस्थ संस्था द्वारा किया गया विधायन प्रत्यायोजित विधायन कहलाता है।
इस प्रकार प्रत्यायोजित विधान का अर्थ हुआ विधान मण्डल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के उपयोग से विधानमण्डल के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधि।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसद के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासनिक कुशलता के लिए वह अपनी विधायनी शक्ति कार्यपालिका के प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित करे। आधुनिक काल में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन निम्नलिखित कारणों से अपरिहार्य हो गया है। यह कारण निम्न प्रकार हैं-
(1) समयाभाव (Lack of Time),
(2) तकनीकी ज्ञान की कमी,
(3) आपात स्थिति,
(4) लचीलापन,
(5) स्थानीय विषय,
(6) अनुभव,
(7) प्रयोगात्मक।
प्रश्न 43. अधीनस्थ विधायन क्या है? What is Subordinate Legislation?
उत्तर- अधीनस्थ विधायन (Subordinate legislation) एक ऐसा विधायन है जो सर्वोच्च शक्ति के अलावा किसी अन्य प्राधिकार सम्पन्न प्राधिकरण या निकाय द्वारा अधिनियमित या निर्मित होता है तथा यह विधायन अपना अस्तित्व या वैधता किसी अन्य सर्वोच्च या उच्चतर प्राधिकारी या प्राधिकरण से प्राप्त करता है। अधीनस्थ विधायन सर्वोच्च या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा संशोधित, परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता है। सामण्ड पाँच प्रकार के अधीनस्थ विधायनों का उल्लेख करते हैं-
(i) औपनिवेशिक विधायन;
(ii) कार्यपालिक या प्रशासनिक विधायन;
(iii) न्यायिक विधायन;
(iv) नगरनिगमीय विधायन;
(v) स्वायत्त विधायन।
प्रश्न 44. ‘पूर्व निर्णय’ से आप क्या समझते हैं? Discuss ‘Precedent’ as a Source of Law.
उत्तर – विधिशास्त्र में विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक पूर्व निर्णय एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। न्यायिक पूर्व निर्णय से तात्पर्य यह है कि जब एक न्यायालय के द्वारा एक विषय पर दिया गया ऐसा निर्णय जो भविष्य में उस विषय एवं उस तरह के मामलों पर एक निश्चित विचारधारा पैदा करे।
पूर्व निर्णय का साधारण शब्दों में अर्थ है- एक ऐसा तरीका जिससे भविष्य में उसी प्रकार के कार्यों को निर्देशित किया जा सके। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने पूर्व निर्णय को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं-
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी – पूर्व-निर्णय एक पूर्ववर्ती उदाहरण की तरह है जो पश्चात्वर्ती मामलों के लिए एक उदाहरण या नियम है।
डायस एवं ह्यजेस के अनुसार– पूर्व-निर्णय से तात्पर्य यह है कि भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूपे में अपनाते हुए भावी निर्णयों को लागू करना।
सामण्ड के अनुसार – पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई सिद्धान्त निहित हो।
इस प्रकार सारांश रूप में कहा जा सकता है कि पूर्व निर्णय एक न्यायालय के द्वारा एक विषय पर दिया गया ऐसा निर्णय है जो भविष्य में उस विषय व उस तरह के मामलों पर एक निश्चित विचारधारा पैदा करता है।
प्रश्न 45. वैध प्रथा या रूढ़ि के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। Discuss the essentials of a valid custom.
उत्तर- वैध रूढ़ि के आवश्यक तत्व (Essential Elements of a Valid Custom)- किसी रूढ़ि को वैधानिक मान्यता प्राप्त होने के लिए उसमें कुछ तत्वों का होना आवश्यक है जो इस प्रकार है-
1. युक्तियुक्तता (Reasonableness)
2. वैध संविधियों से अनुरूपता (Consistency with statute law or conformity)
3. नैतिकता (Morality)
4. निश्चितता (Certainty)
5 अनुपालन (Observance)
6. निरन्तरता तथा स्मरणातीत काल से प्रचलन (Continuity and Immemorial Antiquity)
7. बाध्य शक्ति (Obligatory Force)
8. सार्वभौमिकता (Universality)
सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि एक प्रथा को तभी मान्य माना जा सकता है जब वह ऊपर दिये गये सारे तत्व अपने में रखती हो। उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि रीति-रिवाज तथा व्यक्तिगत विधियों को तय करते समय न्यायाधीश को काफी सावधान रहना चाहिए तथा जैसा भी, जिस रूप में प्रथा को न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए पेश किया जाये, उसी प्रकार उस प्रथा का निर्णय होना चाहिए।
प्रश्न 46. यह कहना कहाँ तक उचित है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं? How for is it correct to say that Judges make Law?
उत्तर- क्या न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं- न्यायालयों को विधि का निर्माण करने की शक्ति है अथवा नहीं, इस विषय में विधिशास्त्रियों में मतभेद है। पहला यह कि न्यायाधीश केवल विद्यमान विधि को घोषित करते हैं और दूसरा यह कि वे विधि का निर्माण करते हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार न्यायाधीशों का कार्य केवल घोषणात्मक है, सृजनात्मक नहीं। न्यायाधीशों द्वारा विवादों के विनिश्चय में पहले से विद्यमान किसी विधि के नियमों का निर्वचन किया जाता है और अपने निर्णय में इन नियमों को समाविष्ट करके उस विधि को घोषित किया जाता है। अतः वे किसी नई विधि का सृजन नहीं करते वरन् किसी विद्यमान विधि का अर्थान्वयन मात्र करते हैं। न्यायिक पूर्व-निर्णय के घोषणात्मक सिद्धान्त के प्रणेता ब्लैकस्टोन हैं जिनके अनुसार न्यायाधीश का कार्य विधि की घोषणा करना है न कि विधि का निर्माण करना।
दूसरे सिद्धान्त के अनुसार न्यायिक पूर्व निर्णय नई विधि का निर्माण करते हैं। इंग्लैण्ड में इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक डायसी थे, जिनका मत है कि इंग्लिश विधि का अधिकांश भाग न्यायाधीशों द्वारा निर्मित किया गया है। ग्रे ने न्यायाधीश को ही विधि का एकमात्र निर्माता माना है।
जब न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले में निर्णय देना होता है जो किसी कानून, रूढ़ि या पूर्वनिर्णय पर आधारित न किया जा सकता हो, तो उसे एक विधिक सिद्धान्त का सूत्रपात करना आवश्यक हो जाता है। परिणामतः उसके द्वारा इस प्रकार दिया गया निर्णय ऐसा होगा जिसका अनुसरण भविष्य में तत्सम वादों में किया जायेगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1976 एस० सी० के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया ‘भावी निराकृति’ सम्बन्धी निर्णय इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूर्व निर्णय सम्बन्धी घोषणात्मक तथा सृजनात्मक सिद्धान्त दोनों में सच्चाई का कुछ अंश विद्यमान है। यथार्थ में पूर्व निर्णय विधि की घोषणा तथा विधि का निर्माण दोनों ही करते हैं। एक ओर वे अस्पष्ट, अनिश्चित तथा बिखरी हुई विधियों को निश्चित, सुस्पष्ट तथा बोधगम्य रूप प्रदान करते हैं, तो दूसरी और वे विधानों द्वारा अधिनिर्धारित विषयों पर निर्णय देते समय विधि का सृजन भी करते हैं। इस प्रकार न्यायाधीश विधियों की कमियों को दूर करते हैं तथा उन्हें बोधगम्य बनाते हैं।
प्रश्न 47. ‘निर्णयाधिकार’ की व्याख्या कीजिए। Discuss the ‘Ratio Decidendi’.
उत्तर – निर्णयाधिकार (Ratio Decidendi)- न्यायिक पूर्व-निर्णय का बाध्यकारी रूप निर्णयाधार होता है। यही पूर्व-निर्णय के सिद्धान्त को भविष्य में रास्ता दिखलाने वाला माना जाता है। निर्णयाधार से अभिप्राय है निर्णय का आधार अर्थात् न्यायिक पूर्व निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाद में निर्णय किस आधार पर दिया गया है। जिस समय एक न्यायाधीश एक मुकदमा तय करता है, उस समय वह उस मुकदमें को वादी के पक्ष में या विपक्ष में तय करता है। वाद तय करते समय वाद में वह सभी कारण देता है जिनकी वजह से वह उस मुकदमें को पक्ष में या विपक्ष में तय कर रहा है। ये कारण ही उस मुकदमें के निर्णयाधार कहलाते हैं और भविष्य में पूर्व-निर्णय (Precedents) बन जाते हैं।
इस प्रकार पूर्व-निर्णय (Precedent) को प्राधिकारिक बनाने वाले न्यायिक सिद्धान्त को निर्णयाधार कहते हैं जिसे न्यायाधीशों द्वारा भविष्य में आनें वाले समवादों में लागू किया जाता है। यह ऐसा विधि नियम होता है जिसे अन्य न्यायालय बन्धनकारी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं।
प्रश्न 48. इतरोक्ति से आप क्या समझते हैं? What do you understand by obiter dicta?
उत्तर- इतरोक्ति (Obiter Dicta) – पूर्व-निर्णय का साधारण रूप प्रासंगिक कथन या इतरोक्ति होता है। विधि की ऐसी अधिघोषणाएँ जो निर्णयाधार का अंश नहीं हैं, इतरोक्ति कहलाती हैं तथा बंधनकारी प्रभाव नहीं रखतीं।
न्यायालय जब अपने तर्क के प्रवाह में किसी ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं जिसे वे अपने किसी विनिश्चय विशेष का आधार नहीं मानते, तो उनके द्वारा किये गये ऐसे प्रतिपादन को इतरोक्ति (Obiter-dicta) कहते हैं अर्थात् इतरोक्ति या प्रासंगिक कथन का तात्पर्य उन बातों से है जो आनुषंगिक रूप में कही जाती हैं। इसका प्रभाव केवल प्रत्ययकारी होता है तथा वे अनुनयात्मक (Persuasive) होते हैं।
कभी-कभी ऐसा होता है कि एक न्यायाधीश जब एक मुकदमें को किसी सारभूत तथ्य पर तय कर रहा है तो उससे मिलते-जुलते किसी समान अन्य प्रश्न पर प्रसंगवश वह अपने विचार व्यक्त करता है तो उस विषय पर व्यक्त किये गये विचारों को प्रासंगिक कथन या इतरोक्ति (Obiter-dicta) कहते हैं।
प्रश्न 49. विधिक अधिकार को परिभाषित कीजिए।Define Legal Right.
उत्तर- विधिक अधिकार- विधिक अधिकारों की परिभाषा और विश्लेषण के बारे में विधिशास्त्रियों में भारी मतभेद हैं। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषायें निम्नलिखित हैं-
सामण्ड के अनुसार – विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो विधि द्वारा संरक्षित हैं।
इहरिंग के अनुसार– विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षति हित है क्योंकि विधि का मूल उद्देश्य मानवीय हितों का रक्षण करते हुए मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को रावना है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि ‘विधिक अधिकार विधिक न्याय हो के एक नियम द्वारा मान्य और रक्षित एक हित है।
प्रश्नन 50 अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। Discuss the different kinds of right.
उत्तर- अधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Rights)- विधिक अधिकारों के निम्न प्रकार हैं-
(1) पूर्वगामी और उपचारी अधिकार
(2) पूर्ण और अपूर्ण अधिकार
(3) सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार
(4) सर्वबन्धी और व्यक्तिबन्धी अधिकार
(5) साम्पत्तिक और व्यक्तिगत अधिकार
(6) स्ववस्तु में अधिकार और परवस्तु में अधिकार
(7) निहित और समाश्रित अधिकार
(8) विधिक और साम्यागत अधिकार
प्रश्न 51. विधिक अधिकार के लक्षण बताइए। State the characteristics of legal rights.
उत्तर-विधिक अधिकार के लक्षण या विशेषताएँ विधिक अधिकार विधिक न्याय ही के एक नियम द्वारा मान्य और रक्षित एक हित है- एक ऐसा हित जिसका अतिक्रमण, उस व्यक्ति के प्रति किया गया एक विधिक दोष होगा और जिसका सम्मान करना एक विधिक कर्त्तव्य है। विधिक अधिकार को मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं-
(1) भोक्ता (The Subject) पोक्ता का अर्थ है. “वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित होता है या जो अधिकार का धारक होता है। बिना एक भोक्ता के कोई अधिकार नहीं हो सकता। अधिकार का भोक्ता नियत या अनियत हो सकता है क्योंकि सम्पूर्ण समाज हो किसी अधिकार का भोक्ता हो सकता है।”
(2) कार्य या प्रविरति (The act or forbearance) अधिकार का सम्बन्ध किसी कार्य या प्रविरति से है। वह किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति में कोई कार्य करने या कार्य से प्रविरत रहने के लिए बाध्य बनाता है जो उस अधिकार के लिए हकदार है। यह अधिकार का तत्व होता है।
(3) अधिकार का विषय या सम्बन्धित वस्तु (The object of right or the resconcerned)- यह यह वस्तु होती है जिसके सम्बन्ध में अधिकार होता है या इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकार का विषय भौतिक (material) या अभौतिक (immaterial) नियत (determinate) या अनियत (indeterminate) हो सकता है।
(4) आबद्ध व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति (The person bound or the person of fincidence)- इसका अर्थ वह व्यक्ति है जिस पर सह-सम्बन्धित कर्त्तव्य होता है।
सामण्ड ने एक पाँचवाँ तत्व भी दिया है, ‘हक’ (title)। वह कहता है कि प्रत्येक विधिक अधिकार में एक हक होता है, अर्थात् कतिपय तथ्य और घटनाएँ जिनके कारण अधिकार उसके स्वामी में निहित हुआ है।
प्रश्न 52. विधिक कर्तव्य को परिभाषित कीजिए।Define Legal duty. Explain the various kinds of duty.
उत्तर- विधिक कर्तव्य (Legal Duties)- सामान्य शब्दों में कर्तव्य (Duty) का अर्थ है-जो एक व्यक्ति को पूरा करना चाहिए अर्थात् एक व्यक्ति के ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करना ही उसका कर्तव्य कहलाता है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार, “संगठित समाज द्वारा निधिक अधिकारों की रक्षा हेतु कार्यों को करने या न करने के जो आदेश दिये जाते हैं, वे आदेश, आदिष्ट व्यक्तियों के लिए विधिक कर्तव्य होते हैं।”
प्रश्न 53. ‘विधिक व्यक्तित्व’ से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Juristic Personality’?
उत्तर- विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality)- विधिक व्यक्तित्व का अर्थ होता है, ‘अधिकार और कर्तव्य धारण करने वाली इकाई’ अर्थात् व्यक्तित्व विधि द्वारा निर्मित एक सत्ता या इकाई (unit) है जिस पर विधि अधिकार और कर्तव्य आरोपित करती है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं पहला प्राकृतिक व्यक्ति जिसका अर्थ है मानव प्राणी। दूसरा विधिक व्यक्ति जिसका अर्थ प्राणी और वस्तुएँ जिनको विधि व्यक्ति मानती है अर्थात् ‘विधिक व्यक्ति’ में वे वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो विधिक प्रयोजन के लिए मानव प्राणी जैसी ही मानी जाती हैं। जैसे-देवता, मूर्ति, निगमित निकाय आदि ऐसी अनेक निर्जीव संस्थायें हैं, जो वास्तविक मनुष्य न होते हुए भी विधिक दृष्टि से ‘व्यक्ति’ माने जाते हैं।
प्रश्न 54. अधिकार एवं कर्त्तव्य परस्पर सहवर्ती हैं। व्याख्या कीजिए। Rights and Duties are correlated. Explain.
उत्तर- अधिकार और कत्र्तव्य में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती (Co-relative) कर्तव्य जुड़ा रहता है। कर्त्तव्य की परिभाषा देते हुए सामण्ड महोदय कहते हैं कि कत्र्तव्य ऐसा बन्धनकारी कार्य होता है जिसका विरोधी शब्द “अपकार” (Wrong) है। प्रोफेसर ग्रे (Gray) के अनुसार कार्यों के “करने” या “न करने” को बाध्यता को ही कर्त्तव्य कहते हैं। विधिक अधिकार (legal rights) ऐसा हित (Interest) है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो विधि द्वारा संरक्षित (Protected) है। सामण्ड कहते हैं “हित” वह है जिसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है तथा जिसको अवहेलना करना अपकार (Wrong) है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा (आशा) की जाती है कि वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरों का कर्त्तव्य होता है क्योंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती (Co-relative) कर्तव्य जुड़ा रहता है। जब विधि यह कहती है कि “प्रत्येक अवयस्क बच्चे का यह अधिकार है कि वह अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करे” तो इसके साथ विवक्षित (Implied) कर्तव्य यह जुड़ा हुआ है कि “प्रत्येक माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने अवयस्क बच्चों का भरण-पोषण करे।”
हालैण्ड के अनुसार कानूनी अधिकार, दूसरों के कार्यों को नियन्त्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे दूसरों को विधिक कर्त्तव्य करने के लिए बाध्य करते हैं। अतः प्रत्येक अधिकार के साथ-साथ दूसरों में निहित कोई एक बराबरी का कत्र्तव्य भी होना चाहिए। क्या इसका उल्टा भी सही है. अर्थात् क्या प्रत्येक कर्तव्य के साथ-साथ उसका बराबरी का कोई अधिकार भो होता है? इस सम्बन्ध में दो मत हैं। प्रथम विचार के अनुसार अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक और संपूरक हैं। दोनों में से किसी एक का भी दूसरे के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्त्तव्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, अतएव इस व्यक्ति में अधिकार निहित होता है। इसी प्रकार अधिकार भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, अतएव उसमें कर्तव्य निहित होता है। प्रत्येक अधिकार या कर्त्तव्य के साथ वैधानिक आभार का बन्धन रहता है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति आपस में सम्बन्धित रहते हैं। सामण्ड कहते हैं कि उस समय तक कर्त्तव्य हो ही नहीं सकता, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति वह हो जिसके लिए यह किया जाता है, इसी प्रकार कोई अधिकार भी नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे अधिकार को प्राप्त करना हो। इस मत के सामण्ड, कीटन तथा पैटन हो प्रमुख समर्थक हैं। पैटन तो यहाँ तक कहते हैं कि अधिकार तथा कर्तव्य में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इनमें से किसी एक की कल्पना पिता के बिना पुत्र की कल्पना करना है।
प्रश्न 55. “व्यक्तित्व मानवता से व्यापक है।” व्याख्या कीजिए। “Personality is wider term than humanity.” Discuss.
उत्तर- व्यक्तित्व मानवता से व्यापक है क्योंकि व्यक्ति के अन्तर्गत न केवल मान आता है अपितु इसके अन्तर्गत कृत्रिम व्यक्ति भी आते हैं यद्यपि वे जीवधारी नहीं होते। देवता, मूर्ति, निगमित निकाय आदि ऐसी अनेक निर्जीव संस्थाएँ हैं जो वास्तविक मनुष्य न होते हुए भी विधिक दृष्टि से व्यक्ति माने जाते हैं अर्थात् इन्हें विधिक व्यक्तित्व (Legal Personality) प्राप्त है।
अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति के लिए ‘Person’ तथा व्यक्तित्व के लिए ‘Personality’ शब्द प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जो इस बात का द्योतक है कि विधिक अधिकारों को रखने की योग्यता तथा कर्तव्यों से युक्त होने की सामर्थ्य, इन दोनों विशेषताओं से युक्त होने वालों को व्यक्ति माना जायेगा।
प्राचीन काल में सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही विधि में व्यक्तित्व रूपी अधिकार प्राप्त थे और अन्य जीवधारी इत्यादि भले ही वे कितने उपयोगी क्यों न रहे हों, उनको विधि का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। धीरे-धीरे यह विचारधारा विकसित हुई कि विधि में सिर्फ एक जीवित शरीरधारी व्यक्ति को ही अधिकार एवं कर्तव्य न दिये जायें बल्कि अन्य प्राणियों, संस्थाओं आदि को भी इस योग्य बनाया जाये। परिणामस्वरूप कम्पनियाँ, निगमों, न्यासों आदि को यह मान्यता दी गई और उन्हें अधिकार व कर्तव्य को रखने की इजाजत दी गई।
सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि विधि में व्यक्ति या व्यक्तित्व का अर्थ है अधिकार एवं कर्तव्यों का वहन करने वाली एक इकाई जिसमें जीवित व अजीवित इकाइयाँ शामिल होती हैं।
प्रश्न 56. अजन्मे व्यक्ति की विधिक स्थिति का वर्णन करें। Describe the legal position of Unborn Person.
उत्तर- अजन्मे व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे बच्चे से है जो माता के गर्भ में आ गया है परन जिसने भौतिक विश्व में अपना अस्तित्व प्रकट नहीं किया है। पैटन के अनुसार, माता के ग में स्थित बच्चा विधिक व्यक्ति नहीं है तथा इसे किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप् नहीं है। यह विचार इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब तक एक बच्चा जीवित जन्म नह ले लेता तथा माता के शरीर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ जाता। उसे विधि के अन्तर्गत को अधिकार प्राप्त नहीं होता। परन्तु यह विचार सही नहीं है। सिर्फ गर्भस्थ शिशु ही नहीं ऐस शिशु जिसने गर्भ धारण नहीं किया है। उसे भी विधिक अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंवि अजन्मे शिशु को अधिकार प्राप्त है तथा ऐसा अधिकार उसे जन्म पर समाश्रित है। समाश्रित अधिकार का स्वामित्व विधिक व्यक्ति को बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। गर्भस्थ शिशु कः उद्देश्यों के लिए व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार एक अजन्मे शिशु के पक्ष में प्रत्यक्ष दान किया जा सकता है। हिन्दू विधि में यदि विभाजन गर्भस्थ शिशु को आबंटित किये बिना किय गया है, जिसे अविभाज्य सम्पत्ति में अंश प्राप्त होता (यदि वह विभाजन की तिथि क अस्तित्व में होता) तो यह विभाजन अपास्त (Setaside) किये जाने योग्य है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के साम्पत्तिक अधिकार (Property right) को विधि में पूर्ण मान्यता प्राप् है।
प्रश्न 57. किन उद्देश्यों के लिए एक मृत व्यक्ति विधिक व्यक्ति माना जाता है? For what purposes a dead person is treated as legal person?
उत्तर- निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक मृत व्यक्ति भी विधिक व्यक्ति माना जाता है, जो इस प्रकार है-
(1) मृत व्यक्ति का शव किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं होता। अतः उसका अंतिम संस्कार उसकी इच्छानुसार किया जाता है। मृत्यु के बाद उसको अधिकार होता है कि उसका दाह-संस्कार सम्मान सहित किया जाये। विधि इस अधिकार की रक्षा करती है।
(2) विधि-मृत व्यक्ति के सम्मान की भी रक्षा करती है। भारतीय दण्ड संहिता में मृत व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या प्रचार करने या उसकी प्रतिष्ठा को झूठी हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है।
(3) मृतक द्वारा की गई वसीयत को विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि के अन्तर्गत मृतक की सम्पत्ति का व्ययन उसके द्वारा वसीयत में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जा सकता है। मृतक के सम्पत्ति व्ययन के अधिकार को मान्यता देना वस्तुतः उसके उत्तराधिकारों के अधिकार को मान्यता देना है क्योंकि सम्पत्ति का प्रयोग उसके उत्तराधिकारी ही करेंगे न कि मृत व्यक्ति स्वयं।
सारांश रूप में कहा जा सकता है कि एक मृत व्यक्ति को विधि में प्राकृतिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता है किन्तु उसके कुप् अधिकार व कर्तव्य उसकी मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं।
प्रश्न 58 क्या भारत का राष्ट्रपति एक विधिक व्यक्ति है? भारत में राष्ट्रपति की वास्तविक विधिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। Whether President of India is a legal person? Explain the real position of the President of India.
उत्तर- हाँ, भारत का राष्ट्रपति एक विधिक व्यक्ति है। भारत में राष्ट्रपति की वास्तविक विधिक स्थिति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को एकल निगम के अन्तर्गत रखा जा सकता है। इससे पद की निरन्तरता पर कोई अन्तर नहीं आता है क्योंकि एक व्यक्ति के पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु होने पर तुरन्त दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण कर लेता है अर्थात् इस पद का वास्तविक अधिकारी एक ऐसा कल्पित व्यक्ति होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती और जीवित पदाधिकारी आते-जाते रहते हैं। इंग्लैण्ड में इस सम्बन्ध में यह सूत्र बड़ा प्रचलित है कि “राजा की कभी मृत्यु नहीं होती है।” अतः भारत का राष्ट्रपति वैध व्यक्ति है।
प्रश्न 59. कब्जा को परिभाषित कीजिए। Define Possession.
उत्तर-कब्जा (Possession)- किसी वस्तु और व्यक्ति के मध्य जो निरन्तर तथा वास्तविक सम्बन्ध रहता है, उसे कब्जा या आधिपत्य (Possession) कहते हैं। यद्यपि ‘कब्जे’ को निश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन है परन्तु कुछ विधिवेत्ताओं ने इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया है-
पोलक ने ‘कब्जे’ को भौतिक नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया है।
सामण्ड के अनुसार, किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच जो निरन्तर तथा वास्तविक सम्बन्ध रहता है, उसे कब्जा कहते हैं। उनके अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे से आशय यह है कि संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु पर कब्जाधारी के विरुद्ध अधिकार न रखे। अतः इससे स्पष्ट है कि सामण्ड ने कब्जे को ‘वस्तु’ से सम्बन्धित माना है, न कि अधिकार से।
जकारिया (Zachariae) के अनुसार ‘कब्जा’ किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच ऐसा सम्बन्ध है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण किये रहने का आशय रखता है तथा उसके व्ययन (Disposal) की क्षमता भी रखता है।
प्रश्न 60. तध्यतः कब्जा एवं विधितः कब्जा। Possession in fact and possession in law.
उत्तर- तथ्यतः तथा विधितः कब्जा (De facto and De jure Possession) किसी व्यक्ति और वस्तु के मध्य जो सम्बन्ध होता है उसे तथ्यतः आधिपत्य (possession in fact) कहते हैं। किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण (physical control) का होना उस वस्तु के तथ्यतः आधिपत्य का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति ने तोते को पिंजरे में रख छोड़ा है तो उस तोते पर व्यक्ति का कब्जा होगा। किन्तु जैसे ही तोता उड़ कर भाग जायेगा उस व्यक्ति का आधिपत्य उस तोते पर से समाप्त हो जायेगा क्योंकि उसका तोते के ऊपर से भौतिक नियंत्रण हट गया।
किसी वस्तु पर तथ्यतः आधिपत्य के लिए व्यक्ति का उस पर भौतिक नियंत्रण का होना तो आवश्यक है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह चौबीस घण्टे उसे अपने नियंत्रण में रखे रहे। मनुष्य का उसके रुपयों पैसों, वस्त्र और मकान आदि पर तब भी आधिपत्य बना रहता है जब वह निद्रा की अवस्था में होता है तथ्यतः आधिपत्य के लिए केवल यह आवश्यक है कि जब वह चाहे अपनी वस्तुओं पर स्वयं का नियंत्रण पुनर्स्थापित कर ले। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को अमुक वस्तु पर अनन्य नियंत्रण (exclusive control) हो और वह इस सम्बन्ध में आश्वस्त हो कि अन्य व्यक्ति उसके वस्तु सम्बन्धी उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति का उस पर तध्यतः कब्जा (Possession in fact) है।
विधितः आधिपत्य (Possession in law) उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति की वस्तु को उसके भौतिक नियंत्रण से छीन लिया जाय और उस व्यक्ति को मुकदमा दायर कर आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार हो। विधि आधिपत्यधारी को संरक्षित करता है उसे पुनः सम्पत्ति का कब्जा प्रदान कर या उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने वाले से क्षतिपूर्ति दिलाकर। मंगल सिंह बनाम श्रीमती रत्ना, AIR (1976) SC 1786 का वाद विधितः आधिपत्य का एक अच्छा उदाहरण है। इस वाद में एक हिन्दू विधवा पति से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पदा पर काबिज थी। 1954 ई० में उसके पति के पट्टीदारों ने कब्जा छीन लिया। इस कारण विधवा ने मंगल सिंह आदि पर कब्जे की पुनः प्राप्ति का वाद दायर किया। जब मुकदमा चल ही रहा था तभी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू हो गया जिसकी धारा 14 (1) यह प्रावधानित करती है कि “हिन्दू नारी के कब्जे में कोई भी सम्पत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामिनी के तौर पर न कि सीमित स्वामिनी के तौर पर धारित की जायेगी।”
अपीलार्थी ने यह तर्क किया कि विवादग्रस्त सम्पदा हिन्दू उत्तराधिकार के लागू होने के समय उनके (विधवा के) कब्जे में थी ही नहीं, अपितु वह उसकी स्वामिनी नहीं हुई। अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि कानून में विधवा उस सम्पत्ति पर उस समय काबिज मानी जायेगी जिस दिन अधिनियम लागू हुआ। न्यायालय ने कहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “कब्जे में” का आशय इतना व्यापक है कि इसमें विधि में कब्जे (Possession in law) के मामले भी आते हैं।
प्रश्न 61. विधि कब्जे को क्यों रक्षण देती है? Why possession is protected by law?
उत्तर – विधिशास्त्रियों के अनुसार कब्जे को संरक्षण दिये जाने के अनेक कारण हैं। विधि केवल वैध कब्जे को ही संरक्षण नहीं देती है अपितु ऐसे कब्जे को भी संरक्षण प्रदान करती है। जो अवैध या अनधिकृत तरीके से प्राप्त किया गया हो। कब्जे का विधि में बहुत महत्व है। इसी कारण से कब्जे को विधि में आरक्षित हित कहा गया है। विधि, कब्जे को संरक्षा देती है,
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
(1) काबिज व्यक्ति की इच्छा की सुरक्षा हेतु- कब्जे में उस व्यक्ति की इच्छा व्यक्त होती है जिसके हाथ में कोई वस्तु है राज्य का कर्तव्य होता है कि वह व्यक्ति की इच्छा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करे इसके साथ-साथ वस्तु की सुरक्षा भी हो जाती है।
(2) कब्जा, स्वामित्व का जनक है- कब्जे को विधि में सुरक्षा इसलिए भी दी जाती है कि यह स्वामित्व का जनक है। बहुत सी परिस्थितियों में कब्जे के आधार पर हो उस वस्तु को स्वामित्व प्राप्त होता है।
(3) व्यक्ति की उन्नति, स्वार्थ एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वस्तुओं के कब्जे को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी होता है।
प्रश्न 62. अमूर्त कब्जा की परिभाषा और उदाहरण दीजिए।Define incorporeal possession and give illustrations.
उत्तर- अमूर्त कब्जा (Incorporeal Possession) वह कब्जा होता है जो वस्तु के साथ अमूर्त रूप से सम्बन्धित होता है। यह किसी वस्तु के ऊपर अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको अमूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता है अपितु महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का अधिकार, पेटेण्ट का अधिकार, गुडविल का अधिकार आदि के अन्तर्गत प्राप्त कब्जा।
प्रश्न 63. विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कब्जे के विभिन्न प्रकारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। Discuss the various kinds of possession recognized by law.
उत्तर- विधि द्वारा मान्यता प्राप्त कब्जे के अनेक प्रकार हैं जिनमें से कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं-
(1) तथ्यतः एवं विधितः कब्जा (De facto and De Jure Possession)
(2) मूर्त एवं अमूर्त कब्जा (Corporeal and Incorporeal Possession)
(3) तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा (Immediate and Mediate Possession)
(4) समवर्ती या दोहरा कब्जा (Concurrent and Duplicate Possession)
(5) कब्जा कल्प (Quasi-Possession)
(6) रचनात्मक कब्जा (Constructive Possession)
(7) प्रयोजनात्मक कब्जा (Derivative Possession)
(8) प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession)
(9) नाम-मात्र कब्जा (Symbolic Possession)
(10) न्यायिक कब्जा (Judicial Possession)।
प्रश्न 64. ऑस्टिन के स्वामित्व का सिद्धान्त क्या है? What is Austin’s theory of ownership?
उत्तर- ऑस्टिन ने ‘स्वामित्व’ की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ‘स्वामित्व’ किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बन्धित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है।
ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
(1) उपयोग की अनिश्चितता (Indefinite in point of use) ऑस्टिन का कथन है कि स्वामित्व का अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु का जिस तरह चाहे उसका इस्तेमाल करे। उसकी इस स्वतन्त्रता पर कोई रोक नहीं है, परन्तु यदि स्वामी चाहे तो आपसी समझौता कर अपने इस अधिकार पर दूसरे द्वारा नियन्त्रण स्वीकार कर सकता है।
(2) व्ययन की दृष्टि में अनिर्बन्धित (Unrestricted to point of disposition) – ऑस्टिन का कहना है कि स्वामित्व दूसरे को अन्तरित किया जा सकता है और यहाँ तक कि उसे इच्छानुकूल खत्म कर सकता है।
(3) अवधि की असीमितता (Unlimited in point of duration)- स्वामित्व को ऑस्टिन ने समय की दृष्टि से असीमित माना है उनके अनुसार स्वामित्व शाश्वत होता है। यह कहना गलत है कि स्वामी की मृत्यु से स्वामित्व समाप्त हो जाता है। स्वामी की मृत्यु पर तत्काल स्वामित्व उसके उत्तराधिकारियों में न्यस्त हो जाता है। वसीयत के द्वारा ही स्वामी अपनी वस्तु को मृत्यु के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है।
प्रश्न 65. सह-स्वामित्व पर टिप्पणी लिखें। Write short notes on co-ownership.
उत्तर – सह-स्वामित्व (Co-ownership)- जब स्वामित्व का अधिकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित हो तो उस दशा में प्रत्येक का स्वामित्व सह- स्वामित्व कहा जायेगा।
सह स्वामित्व दो प्रकार का होता है-
(i) सामान्य स्वामित्व (Ownership in Common)
(ii) संयुक्त स्वामित्व (Joint Ownership) 1
(i) सामान्य स्वामित्व (Ownership in Common)- जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं; सामान्य स्वामित्व कहलाता है। इसमें कब्जा अविभाजित रहता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सह-स्वामियों के साथ उस भूमि या वस्तु का स्वामी होता है।
(ii) संयुक्त स्वामित्व (Joint Ownership)- संयुक्त स्वामित्व में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर या जुड़कर किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं। संयुक्त स्वामित्व में किसी सह-स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है।
प्रश्न 66. सम्पत्ति के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। Explain the classification of property.
उत्तर-सम्पत्ति का वर्गीकरण- सम्पत्ति को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(1) मूर्त तथा अमूर्त सम्पत्ति,
(2) चल तथा अचल सम्पत्ति,
(3) भौमिक तथा वैयक्तिक सम्पत्ति,
(4) लोक एवं निजी सम्पत्ति।
(1) मूर्त (Corporeal) तथा अमूर्त (Incorporeal) सम्पत्ति – मूर्त (Corporeal) सम्पत्ति वह है जिसकी अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हो सकती है, जो छुई जा सकती हो या देखी जा सकती हो, जैसे भूमि, भवन, पुस्तक, बर्तन, आभूषण आदि। जिस सम्पत्ति की अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों से नहीं हो सकती, उसे अमूर्त (Incorporeal) सम्पत्ति कहते हैं, जैसे, कापीराइट, ट्रेडमार्क, सुखाधिकार (easement) आदि।
(2) चल तथा अचल सम्पत्ति- जो सम्पत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके वह चल (moveable) सम्पत्ति और जो ऐसी न हो वह अचल (Immovable) सम्पत्ति कहलाती थी।
(3) भौमिक तथा वैयक्तिक सम्पत्ति (Real and Personal Property)- इंग्लैण्ड में सम्पत्ति का विभाजन दो भागों में किया जाता है- भौमिक एवं व्यक्तिगत। यह भेद अचल एवं चल सम्पत्ति की ही तरह का है। भूमि सम्बन्धी समस्त अधिकार भौमिक (Real) सम्पत्ति कहलाते हैं तथा चल सम्पत्ति को वैयक्तिक सम्पत्ति (Personal Property) कहा जाता है।
(4) लोक या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्ति (Public and Private Property)- जहाँ तक स्वामित्व का सम्बन्ध है सम्पत्ति सार्वजनिक या निजी हो सकती है। लोक सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जो लोक (सार्वजनिक) रूप से सरकारी सक्षमता में सार्वजनिक रूप से धारण की जाती है। इससे स्पष्ट है कि निजी सम्पत्ति यह है जो व्यक्तिगत सक्षमता या हैसियत (capacity) में किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है।
प्रश्न 67. भारतीय संविधान में सम्पत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? What is the constitutional position of right of property?
उत्तर- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पहले सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद-19 (च) और अनुच्छेद-31 के तहत मौलिक अधिकार था किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद यह मौलिक अधिकार समाप्त करके इस अधिकार को सांविधानिक अधिकार बना दिया गया जिसका विनियमन, अब साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है इसके लिए सांविधानिक संशोधन की आवश्कयता नहीं होगी। सम्पत्ति के अधिकार को एक सांविधानिक अधिकार के रूप में बनाये रखने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 (क) जोड़ा गया है।
अनुच्छेद 300 (क) यह उपबन्धित करता है कि “कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।”
नये अनुच्छेद 300 (क) के अधीन किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को राज्य द्वारा अर्जित किये जाने के लिए केवल एक शर्त है और वह है विधि का प्राधिकार। किस उद्देश्य के लिए तथा क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया जायेगा और दिया जायेगा तो कितना दिया जायेगा, इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन होगा। इस संशोधन के फलस्वरूप अब भाग-3 में प्रदत्त मूल अधिकारों और अनुच्छेद 300 (क) के अधीन सम्पत्ति के सांविधानिक अधिकारों में अन्तर केबल इतना है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय में जा सकते हैं जबकि किसी व्यक्ति की अनुच्छेद 300 (क) के अधीन सम्पत्ति के सांविधानिक अधिकार के राज्य द्वारा उल्लंघन किये जाने की दशा में अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय से उपचार नहीं माँग सकता है। वह केवल अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में ही जा सकता है।
प्रश्न 68. स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। Define ownership.
उत्तर- स्वामित्व (Ownership) – स्वामित्व की परिभाषा ऑस्टिन के अनुसार, “स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बन्धित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है।” हॉलैण्ड ने भी इसी परिभाषा को अपनाया है उनके अनुसार, “किसी वस्तु पर पूर्ण नियन्त्रण ही स्वामित्व है।” सामण्ड महोदय ऑस्टिन की परिभाषा से सहमत नहीं हैं। सामण्ड कहते हैं कि “स्वामित्व व्यापक रूप में व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को किसी वस्तु पर प्राप्त अधिकार के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है।” इसके अनुसार स्वामित्व में सभी प्रकार के अधिकार एम्मिलित होते हैं चाहे वे साम्पत्तिक हों या व्यक्तिगत, स्वसाम्पत्तिक हों या परसाम्पत्तिक, चाहे वे सार्वभौमिक (Right in rem) हों या व्यक्तिलक्षी (Right in personam)।
प्रश्न 69. स्वामित्व एवं कब्जे में अन्तर स्पष्ट करें। Distinguish between ownership and possession.
उत्तर – स्वामित्व एवं कब्जे में अन्तर –
स्वामित्व (Ownership)
(1) स्वामित्व का अधिकार श्रेष्ठ तथा व्यापक है।
(2) स्वामित्व का अधिकार स्वत्व (Title) का अधिकार है। यह आवश्यक रूप से उपयोग का अधिकार नहीं है क्योंकि किसी सम्पत्ति पर स्वामित्व एक व्यक्ति का हो सकता है कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता है।
(3) स्वामित्व के अधिकार में कब्जे का अधिकार सम्मिलित होता है।
(4) स्वामित्व का सम्बन्ध विधि से है।
(5) स्वामित्व का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है।
कब्जा या आधिपत्य (Possession)
(1) कब्जा स्वामित्व से निम्नतर अधिकार है यह स्वामित्व के अन्तर्गत आता है।
(2) कब्जे का अधिकार आवश्यक रूप से उपभोग का अधिकार है।
(3) आधिपत्य या कब्जे के अधिकार में स्वामित्व का अधिकार सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है।
(4) आधिपत्य या कब्जे का सम्बन्ध तथ्य से है।
(5) आधिपत्य या कब्जे का अधिकार स्वामित्व की अपेक्षा निम्न स्तर (inferior) का अधिकार है।
प्रश्न 70. आभार से आप क्या समझते हैं? What do you understand by obligation?
उत्तर- आभार (Obligations)- सामण्ड के अनुसार, यह केवल कर्तव्य का ही द्योतक नहीं है इससे सम्बन्धित अधिकार का भी आभास मिलता है। यह सिक्के के दो पहलू ‘के समान है। धारक की दृष्टि से यह अधिकार है और उससे बद्ध होने वाले की ओर से देखने पर कर्तव्य। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधता है।
सैविनी के अनुसार- ‘आभार दूसरे व्यक्ति के ऊपर नियन्त्रण है फिर भी उसके शरीर पर समीक्षा मायनों में नहीं। जिसमें उसका व्यक्तित्व इच्छित होगा किन्तु उसके कार्यों पर जो उसकी स्वतन्त्र इच्छा से निकालकर हमारी इच्छा के अधीन समझी जाती है। काण्ट कहते हैं यह बतौर इसे निर्धारित करने के साधन के रूप में मेरी ही इच्छा के माध्यम से, एक निश्चित कार्य के बाबत स्वतन्त्रता की विधि के अनुसार दूसरे की इच्छा का कब्जा है।
प्रश्न 71. विधि से क्या अभिप्रेत है? What is meant by Law?
उत्तर- विधि (Law) – विधि की एक सर्वमान्य परिभाषा में उन सभी तत्वों का विद्यमान होना अपेक्षित है, जो तत्पश्चात् वर्णित विभिन्न भावों को दर्शाते हों। मानव-समाज में व्यक्तियों के संव्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा नियम बनाये जाते हैं, जिन्हें ‘विधि’ कहा जाता है। इसी कारण विधि को सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रमुख साधन माना गया है। हेनरी सिडविक के अनुसार, ‘विधि’ शब्द का प्रयोग किसी ऐसे सामान्य नियम के लिए किया जा सकता है जो किन्हीं कार्यों को करने अथवा न करने का आदेश देता हो और जिसकी अवज्ञा करने पर दोषी व्यक्ति को दण्ड भोगना पड़े।
विधि की निश्चित परिभाषा में एक अन्य कठिनाई यह है कि यह सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित होने के कारण सदैव परिवर्तनशील होती है और सामाजिक बदलाव के साथ-साथ स्वयं को परिमार्जित करती रहती है तथापि विधि के अर्थ को समझने की दृष्टि से विधिशास्त्रियों द्वारा दी गई विधि की परिभाषाएँ निम्न हैं-
हालैण्ड के अनुसार, विधि से आशय मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है, जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरणों द्वारा होती है और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किये जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई व्यक्ति होता है जिसे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो कि राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं।
सामण्ड के अनुसार सामान्य अर्थ में विधि के अन्तर्गत सभी कार्यों सम्बन्धी नियमों का समावेश है। उनका कथन है कि विशिष्ट अर्थ में विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है जो किसी देश के नागरिकों के प्रति लागू होती है। सामण्ड इसे राज्य की विधि, वकीलों की विधि और न्यायालयी विधि कहते हैं। उनके अनुसार वास्तव में विधिशास्त्रीय विधि वही है जो न्याय की स्थापना के लिए न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है।
ऑस्टिन ने विधि को सम्प्रभुताधारी या राजनीतिक दृष्टि से उच्चतर व्यक्तियों द्वारा शासित व्यक्तियों पर अधिरोपित किये गए नियमों का समूह निरूपित किया है। ये नियम व्यक्तियों से एक निश्चित आचरण की अपेक्षा करते हैं, जिनके लिए शासित वर्ग कर्तव्यबद्ध है तथा इनके पीछे सम्प्रभु की शास्ति होती है। इसे ऑस्टिन ने ‘पॉजिटिव लॉ’ कहा है।
डीन रास्को पाउण्ड ने ‘विधि’ शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया है-
(1) प्रथम अर्थ में ‘विधि’ एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी राजनीति के सुसंगठित समाज में मानव आचरणों को सामाजिक नियन्त्रण में रखा जाता है।
(2) दूसरे अर्थ में विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शन का कार्य करती है।
(3) तीसरे अर्थ में विधि के अन्तर्गत देश की सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएँ समाविष्ट हैं।
संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि डीन रास्को पाउण्ड देश की सामान्य विधि प्रणाली को ही ‘विधि’ के रूप में स्वीकार करते हैं। पाठण्ड के अनुसार ‘विधि’ और ‘नैतिकता’ का उद्गम स्रोत एक ही होता है किन्तु उनके विकास की क्रिया में भिन्नता होती है। नैतिकता का सम्बन्ध मनुष्य की अन्तरात्मा से होता है जबकि विधि का प्रयोजन मनुष्य के बाह्य आचरणों को नियन्त्रित करना है।
प्रश्न 72. शक्ति की परिभाषा दीजिए। Define Power.
उत्तर- शक्ति की परिभाषा – विधिशास्त्री सामण्ड के अनुसार, विधि द्वारा किसी को दी जाने वाली क्षमता का नाम ‘शक्ति’ (might) है, जिसके द्वारा वह अपने या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों या अन्य विधिक सम्बन्धों को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित कर सकता है।
जो शक्ति विधि सम्बन्ध स्थापित करती है तो उसे सत्ता (अथॉरिटी) कहते हैं और जब अपने ही ऊपर लागू होती है तो क्षमता कहलाती है। शक्ति दो प्रकार की हो सकती हैं- (1) सार्वजनिक (Public); तथा (2) प्राइवेट (Private) ।
सार्वजनिक शक्ति तो राज्य के प्रतिनिधियों को मिली हुई होती है, जैसे न्यायाधीशों को प्राप्त शक्ति। व्यक्तिगत शक्ति लोगों को आमतौर पर मिली होती है।
प्रश्न 73. स्वत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। Write a short comment on Title.
उत्तर – स्वत्व (Title) – प्रत्येक विधिक अधिकार का एक स्वत्व होता है। यह कतिपय तथ्यों या घटनाओं से सम्बन्धित होता है, जिसके जरिये अधिकार अपने स्वामी में निहित होता है।
सामण्ड ने विधिक अधिकारों के जो पाँच लक्षण स्वीकार किये हैं उनमें से एक अधिकार का स्वत्व (Title of right) भी है। सामण्ड द्वारा स्वीकार किये गये विधिक अधिकार के पाँच लक्षण हैं-
(1) अधिकार का धारणकर्ता या हकदार व्यक्ति ।
(2) अधिकार से आबद्ध व्यक्ति।
(3) अधिकार की अन्तर्वस्तु।
(4) अधिकार की विषयवस्तु ।
(5) अधिकार का स्वत्व (Title of the right) 1
सामण्ड के अनुसार अधिकार के स्वामी की स्थिति के अनुसार त्रिपक्षीय सम्बन्ध उत्पन्न होता है-
(1) यह कतिपय व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार है।
(2) यह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी कार्य या कार्य लोप से सम्बन्धित एक अधिकार है; और
(3) यह किसी वस्तु के ऊपर या उसके सम्बन्ध में एक अधिकार है जिससे वह कार्य या कार्यलोप सम्बन्धित है।
हॉलैण्ड ने स्वत्व के तत्व को विधिक अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं माना है।
‘कीटन’ (Keeton) ने भी स्वत्व को केवल अधिकार का साक्ष्य या स्रोत माना है।
स्वत्व (Title) का मूलतः अर्थ है एक मार्क (A mark), साइन (sign) अथवा इन्सक्रिप्सन (inscription) उदाहरण के लिए किताब का स्वत्व (Title)।
स्वत्व (Titles) दो प्रकार का होता है-
(1) मूल (Original); अथवा
(2) व्युत्पन्न (Derivative) I
पहला वे स्वत्व हैं जो डि नोवो (de novo) का सृजन करते हैं। दूसरा वह है जो वर्तमान अधिकार के अस्तित्व को नये स्वामित्व में बदलता है अर्थात् ऐसे तथ्य जो अधिकार का सृजन या पुनः प्रारम्भ करते हैं, तो मूल हक (Original Title) कहलाते हैं। परन्तु वे किसी पूर्व से ही विद्यमान अधिकार का किसी अन्य में अन्तरण करते हैं तो व्युत्पन्न हक कहलाते हैं।
प्रश्न 74. विधि के मूल मानकत्व सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। Discuss Grund Norm theory of law.
उत्तर- केल्सन के अनुसार, विधिशास्त्र, मानकों या नियमों का विज्ञान है। इन मानकों की वैधता की कसौटी के रूप में केल्सन मूल नियमों या मौलिक मानकों (Grund Norms or Fundamental Norms) को देखता है। केल्सन के अनुसार, सभी मानक (Norms) या नियमों की वैधता को मौलिक मानक की कसौटी पर परीक्षित करना चाहिए। यदि कोई मानक (Norm) या नियम मूल मानक या मौलिक नियम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह मानक (Norm) वैध मानक न होकर अवैध मानक या अवैध नियम होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि यह मूल मानक या मौलिक नियम का पता कैसे लगाया जाय। किसी विधि व्यवस्था में मूल मानक या मौलिक नियम (Grund Norm) को सुनिश्चित करना कठिन है। मौलिक मानक का व्यकलन (Deduction of Grund Norm) विधि विज्ञान के किसी भी शुद्ध सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। यह प्रारम्भिक परिकल्पना का तार्किक सबूत नहीं दिया जा सकता। इंग्लैण्ड के लिए संसद के माध्यम से जिस विधि का निर्माण सम्राट करता है, वह मौलिक मानक है तथा इंग्लैण्ड के विधिक मानक इस मौलिक मानक की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। हम ऐतिहासिक रूप से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस सिद्धान्त को इंग्लैण्ड में कैसे स्वीकार किया गया परन्तु हम उसे शुद्ध तर्कों द्वारा प्रदर्शित या साबित नहीं कर सकते। इन मौलिक मानकों एवं नियमों का प्राथमिक उद्देश्य है कि यह राज्य में कुछ व्यक्तियों को मानकों के निर्माण को क्षमता प्रदान करता है, जो मानकों के निर्धारण की प्रक्रिया का प्रतिपादन करें। इस आधारभूत या मौलिक मानक से मानक निर्माण की शक्ति निचले स्तर पर प्रवाहित होती है जो एक स्तर (Stage) से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होती है। प्रत्येक स्तर पर निर्मित मानकों की वैधता की परख मौलिक मानक की कसौटी पर ही होगी। विधि निर्माण या मानक निर्माण के विभिन्न स्तर संयुक्त रूप से किसी राष्ट्र की विधिक व्यवस्था का निर्माण करती है। मानकीय विज्ञान का यह सिद्धान्त सार्वभौमिक है तथा किसी भी विधिक व्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है। चूंकि यह सिद्धान्त एक विशिष्ट विधिक व्यवस्था के लिए सीमित न होकर सभी विधिक व्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है। अतः केल्सन अपने इस सिद्धान्त को विधि का विशुद्ध सिद्धान्त (Pure Theory of Law) कहता है।
प्रश्न 75. दायित्व से आप क्या समझते हैं? What do you understand by ‘Liability’?
उत्तर- व्यापक अर्थ में दायित्व का अर्थ है “न्यायिक बन्धन”। किसी व्यक्ति का दायित्व उस समय उद्भूत होता है जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार अपकारकर्ता (wrong-doer) अपने अपकृत्य (wrong) के लिए उत्तरदायी होता है। विधिशास्त्री सामण्ड अपनी पुस्तक, ‘ज्युरिस्प्रूडेन्स’ में कहते हैं-
“A man’s liability consists in those things which he must do or suffer because he has already failed in doing what he thought.”
किसी मनुष्य के दायित्व में वे बातें होती हैं जिनके परिणामस्वरूप भुगतान या यातना सहनी चाहिए, क्योंकि यह उस कार्य को करने में असफल रहा जो उसे करना चाहिए था।
संक्षेप में दायित्व की उत्पत्ति तभी होती है जब कोई अपकार (Wrong) किया जाय और इसका अस्तित्व अपकारकर्ता और अपकार के बीच होता है।
प्रश्न 76. दीवानी और आपराधिक दायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। Write short notes on civil and criminal liability.
उत्तर- दीवानी (Civil) दायित्व का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपकारी द्वारा अपकारित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाये। अतः दीवानी मामलों में प्रतिवादी के दायित्व का निर्धारण करते समय अपकार करने में उसके उद्देश्य या हेतु की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में, साधारणतः सिविल विधि में न्यायालय इस ओर ध्यान नहीं देता कि प्रतिवादी ने अपकृत्य आशय सहित किया है या उससे वह अपकृत्य अनजाने में हो गया या वह उसकी असावधानी के कारण हुआ है। दीवानी विधि का उद्देश्य तो केवल यह है कि यदि प्रतिवादी के अपकृत्य के कारण वादी को क्षति हुई है, तो प्रतिवादी वादी की क्षतिपूर्ति कर दे।
आपराधिक दायित्व (Criminal Liability) – जब कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता या किसी आपराधिक अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित कोई कार्य या चूक करता है तो उस पर आपराधिक दायित्व हो जाता है। आपराधिक विधि का उद्देश्य है अपराधों को रोकना और शान्ति व्यवस्था बनाये रखना। आपराधिक दायित्व के अन्तर्गत दण्ड देने के सम्बन्ध में तीन तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है- (1) अपराध का आशय, (2) अपराध की सीमा, (3) अपराध की प्रकृति ।
प्रश्न 77. ‘सम्पत्ति’ शब्द को परिभाषित कीजिए। Define the term ‘Property’.
उत्तर – सम्पत्ति (Property)- सम्पत्ति एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर आधिपत्य का ऐसा अधिकार हो जो दूसरे के आधिपत्य के अधिकार को अपवर्जित करता हो तो यह कहा जायेगा कि वह वस्तु उस व्यक्ति की सम्पत्ति है जिसका उस पर अपवर्जनकारी (Exclusive) आधिपत्य है। सम्पत्ति का अधिकार यदि एक व्यक्ति के पक्ष में है तो वह सर्वश्रेष्ठ आधिपत्य का अधिकार है। यह अधिकार आत्यन्तिक तथा अपवर्जनकारी होना चाहिए अर्थात् वस्तु पर आधिपत्य का अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो उस वस्तु को अपनी सम्पत्ति कहता है। सम्पत्ति किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार है जिसे अन्य व्यक्ति से चुनौती न मिले। सम्पत्ति सभी समाज में व्यक्तियों के हितों का केन्द्र (Centre of interest) रहा है और रहेगा।
प्रश्न 78 विधि एवं नैतिकता में भेद। Difference between law and morality.
उत्तर- विधि एवं नैतिकता में अन्तर – विधि और नैतिकता के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि समाज के विकास के प्रारम्भिक युग में इन दोनों में कोई विभेद नहीं था। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में धर्म के अन्तर्गत नैतिकता और विधि दोनों का ही पर्याप्त अंशों में समावेश था तथा प्राचीन समुदायों में प्रथा और परम्पराओं के द्वारा मनुष्यों के आचरण नियंत्रित होते थे परन्तु राज्य को उत्पत्ति के पश्चात् विधि और नैतिकता में भेद निरन्तर बढ़ता गया और वर्तमान में ये दोनों एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न माने जाते हैं। विधि का सम्बन्ध मानव के बाह्य संव्यवहारों में से ही है आंतरिक विचारों से नहीं परन्तु दूसरी ओर नैतिकता का मनुष्य की अंतरात्मा से सम्बन्ध है। अतः कानून नैतिकता पर आधारित नहीं है। नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्तियों की उचित और अनुचित की भावना से है। दूसरे, विधि वस्तुनिष्ठ तथा निश्चयात्मक होती है। विधि समायोजित होती है। ऐसे अनेक कृत्य हैं जो अनैतिक न होते हुए भी अपराध घोषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बिना लाइसेंस के स्कूटर या कार चलाना कानूनन अपराध है यद्यपि इसमें अनैतिकता जैसी कोई बात नहीं है।
विधि का अनुपालन दण्ड के भय से किया जाता है, अर्थात् विधि के पीछे बाह्य शक्ति होती है, परन्तु नैतिकता के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। अतः किसी संविदा को भंग करने वाले को राज्य द्वारा दण्डित किया जा सकता है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो केवल इसके लिए राज्य उसे दण्डित नहीं कर सकता।
भारतीय विधि में नैतिकता और सदाचार को आज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एस० सी० गुप्ता तथा अन्य बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1982 सु० को० के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में भर्तृहरि के ‘नीति शतक’ में उल्लिखित आदशों को उद्धृत करते हुए अवलोकन किया-
“नीतिशास्त्र और सदाचार में निपुण व्यक्ति अनादर करे या आदर, धन संग्रहीत हो या लुप्त हो जाए, मृत्यु आज ही आ जाए या एक युग के पश्चात् सद्विवेकशील व्यक्ति अपने सदाचरण के मार्ग से विचलित नहीं होता।”
इस विनिश्चय से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विधि में नैतिकता और सदाचार को आज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विधि तथा नैतिकता का उद्गम स्रोत एक ही है। लेकिन उनके विकास में भिन्नता है। यही कारण है कि अधिकांश विधियों में नैतिकता या नीति आचार का थोड़ा बहुत अंश अवश्य रहता है तथा जो कृत्य विधि विरुद्ध होते हैं वे अधिकतर अनैतिक भी माने जाते हैं उदाहरणार्थ हत्या, चोरी, लूटपाट, बलात्संग आदि सभी के विरुद्ध अपराध अनैतिक भी है।
********