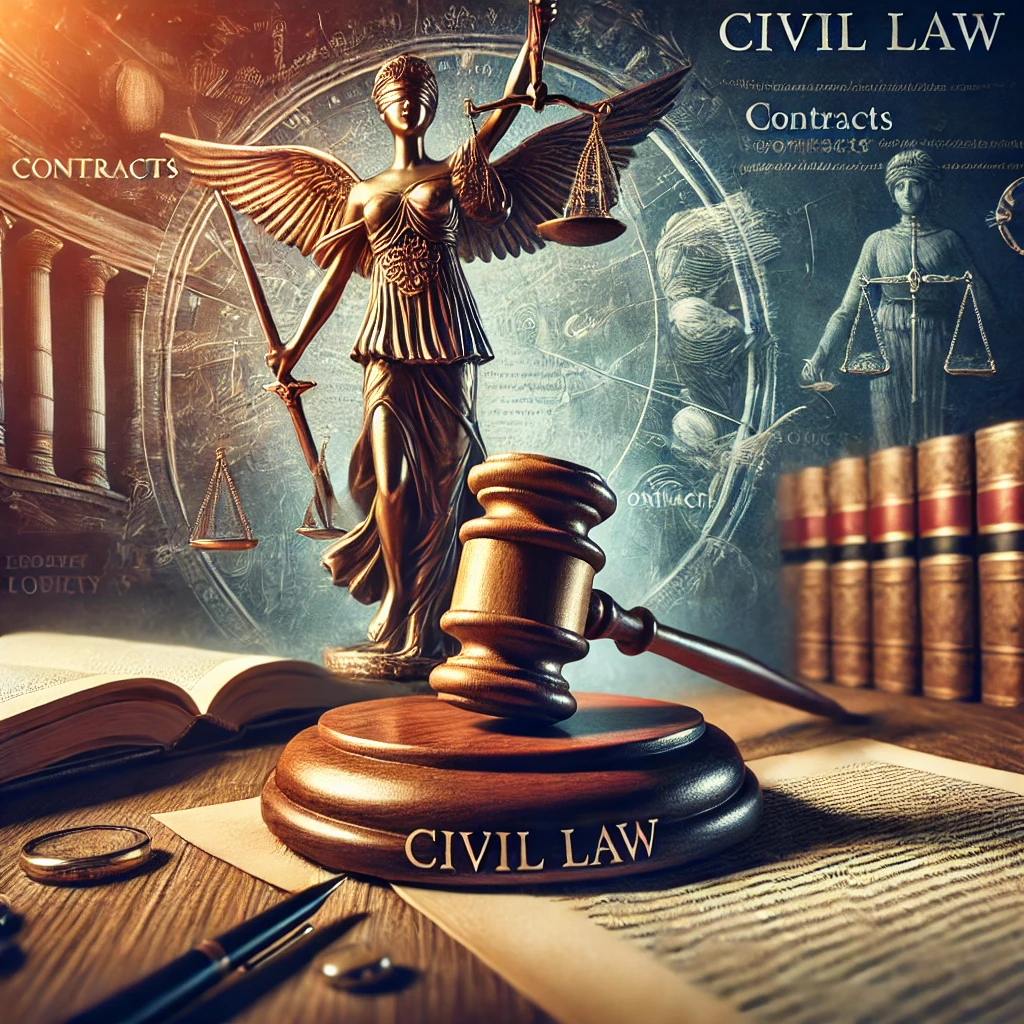सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) : 1908
1. सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) 1908 क्या है?
सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 (CPC) भारत का एक प्रमुख प्रक्रियात्मक कानून है, जो सिविल मामलों की सुनवाई और उनके निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई मुकदमा कैसे दायर किया जाए, उसका उत्तर कैसे दिया जाए, गवाह और साक्ष्य कैसे पेश किए जाएँ, न्यायालय का निर्णय कैसे लागू किया जाए, और अपील या पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी। यह कोड पूरे भारत में लागू है (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, वहाँ अलग से प्रावधान हैं)। CPC दो भागों में विभाजित है – धाराएँ (Sections) और ऑर्डर्स व नियम (Orders & Rules)। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह न्यायालयों को एक समान प्रक्रिया प्रदान करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
2. धारा 9 CPC का महत्व क्या है?
धारा 9 CPC सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है। सामान्य नियम यह है कि जहाँ भी किसी व्यक्ति का सिविल अधिकार प्रभावित होता है, वहाँ सिविल न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार होगा। केवल वही मामले सिविल न्यायालय में नहीं सुने जाएँगे, जिन्हें विशेष रूप से किसी अन्य कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को अपने नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का अवसर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि “सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और केवल उन्हीं मामलों में सीमित होगा, जहाँ किसी अन्य कानून ने इसे स्पष्ट रूप से समाप्त किया हो।”
3. Res Judicata (धारा 11) क्या है?
Res Judicata का अर्थ है – पहले से तय किए गए विवाद को पुनः नहीं उठाया जा सकता। CPC की धारा 11 के अनुसार, यदि किसी विवाद पर पहले ही सक्षम न्यायालय अंतिम निर्णय दे चुका है, तो वही विवाद दोबारा किसी अन्य मुकदमे में उठाया नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य मुकदमों की संख्या को नियंत्रित करना और न्यायिक अनुशासन बनाए रखना है। केस – Satyadhyan Ghosal v. Deorajin Debi (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Res Judicata का सिद्धांत न्याय की स्थिरता और अंतिमता के लिए आवश्यक है।
4. Res Sub Judice (धारा 10) क्या है?
धारा 10 CPC Res Sub Judice का सिद्धांत स्थापित करती है। इसका अर्थ है – यदि किसी मुद्दे पर पहले से ही कोई मुकदमा विचाराधीन (Pending) है, तो उसी मुद्दे पर समान पक्षकारों के बीच दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय दूसरे मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। इसका उद्देश्य है कि एक ही विषय पर अलग-अलग निर्णय न हों और न्यायालय का समय बच सके।
5. धारा 80 CPC के अंतर्गत सरकारी मुकदमों से पूर्व नोटिस का प्रावधान क्या है?
धारा 80 CPC के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के विरुद्ध अपने पद के कारण उत्पन्न विवाद पर वाद दायर करना चाहता है, तो उसे दो माह पूर्व लिखित नोटिस देना आवश्यक है। इस प्रावधान का उद्देश्य है सरकार को विवाद का समाधान अदालत से बाहर करने का अवसर देना। हालाँकि, यदि मामला तात्कालिक (Urgent) हो तो न्यायालय बिना नोटिस के भी मुकदमा स्वीकार कर सकता है।
6. धारा 89 CPC का महत्व क्या है?
धारा 89 CPC न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे मामलों को वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR) के लिए भेज सकें। इसमें Arbitration, Conciliation, Mediation और Lok Adalat शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि छोटे-मोटे विवाद जल्दी और सस्ते तरीके से निपट जाएँ तथा न्यायालयों का भार कम हो। केस: State of Punjab v. Jalour Singh (2008) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 89 CPC के महत्व को स्वीकार किया।
7. अपील (Appeal) और पुनरीक्षण (Revision) में अंतर बताइए।
- अपील (Appeal): अपील का अर्थ है – किसी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च अदालत में पुनः सुनवाई की मांग करना। CPC में प्रथम अपील (धारा 96) और द्वितीय अपील (धारा 100) का प्रावधान है।
- पुनरीक्षण (Revision): यदि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर आदेश पारित करती है, तो उच्च न्यायालय धारा 115 CPC के अंतर्गत उसकी समीक्षा कर सकता है।
- अंतर: अपील में पूरे मामले की पुनः सुनवाई होती है, जबकि पुनरीक्षण केवल अधिकार क्षेत्र और कानून की त्रुटियों की जाँच के लिए होता है।
8. अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) क्या है?
Order XXXIX CPC अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) से संबंधित है। यह एक अंतरिम आदेश होता है, जो न्यायालय मुकदमे की लंबित स्थिति में किसी पक्ष को किसी कार्य से रोकने के लिए देता है। इसका उद्देश्य है कि अंतिम निर्णय आने तक स्थिति यथावत बनी रहे और किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति न हो। उदाहरण: यदि संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद है, तो अदालत किसी पक्ष को उस संपत्ति को बेचने से रोक सकती है।
9. Decree और Order में अंतर बताइए।
- Decree (डिक्री): न्यायालय का औपचारिक निर्णय, जिसमें मुकदमे के सभी मुद्दे तय कर दिए जाते हैं। यह न्यायालय का अंतिम आदेश होता है।
- Order (आदेश): न्यायालय का वह निर्णय, जो मुकदमे के दौरान किसी एक मुद्दे पर दिया जाता है, लेकिन यह अंतिम न होकर सहायक हो सकता है।
- अंतर: डिक्री अंतिम निर्णय है, जबकि आदेश मध्यवर्ती निर्णय भी हो सकता है।
10. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ (Inherent Powers – धारा 151) क्या हैं?
धारा 151 CPC न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह न्याय हित में कोई भी आदेश पारित कर सकता है, भले ही वह CPC की किसी धारा या नियम में स्पष्ट रूप से न लिखा हो। इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाता है जब CPC का कोई अन्य प्रावधान उपलब्ध न हो। केस: Manohar Lal Chopra v. Rai Bahadur Rao Raja Seth Hiralal (1962) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालत अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग कर अंतरिम निषेधाज्ञा दे सकती है।
11. Plaint क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं?
Plaint वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा वादी (Plaintiff) अपना दावा न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है। यह मुकदमे की शुरुआत का आधार होता है। Order VII CPC में Plaint से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
आवश्यक तत्व:
- पक्षकारों के नाम और पता।
- कारण-ए-दावा (Cause of Action)।
- न्यायालय का अधिकार क्षेत्र।
- विवादित संपत्ति/मुद्दे का विवरण।
- वादी की प्रार्थना (Relief Claimed)।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न।
यदि Plaint में आवश्यक तत्व न हों, तो न्यायालय उसे अस्वीकार (Rejection of Plaint) भी कर सकता है।
12. Written Statement क्या है?
Written Statement प्रतिवादी द्वारा Plaint का उत्तर होता है। यह Order VIII CPC के अंतर्गत दायर की जाती है। इसमें प्रतिवादी वादी के आरोपों का खंडन करता है और अपने बचाव के लिए तथ्य प्रस्तुत करता है।
विशेषताएँ:
- Plaint के प्रत्येक कथन का स्वीकार या अस्वीकार।
- प्रतिवादी का अपना संस्करण।
- यदि कोई Counter-Claim या Set-Off हो तो उसका उल्लेख।
न्यायालय सामान्यतः Written Statement दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय देता है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 90 दिन तक किया जा सकता है।
13. Set-Off और Counter-Claim में अंतर बताइए।
- Set-Off: जब प्रतिवादी, वादी से किसी धनराशि का दावा करता है और उसे वादी के दावे के विरुद्ध समायोजित करना चाहता है। यह केवल धन के मामलों में लागू होता है।
- Counter-Claim: प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र दावा करना। यह केवल धन तक सीमित नहीं बल्कि अन्य अधिकारों पर भी आधारित हो सकता है।
अंतर: Set-Off एक रक्षात्मक दावा है, जबकि Counter-Claim एक आक्रामक (Offensive) दावा है।
14. Framing of Issues (Order XIV) का उद्देश्य क्या है?
Order XIV CPC के अंतर्गत अदालत मुकदमे में उठाए गए विवादित प्रश्नों (Issues) को तय करती है।
उद्देश्य:
- मुकदमे की सीमाएँ निर्धारित करना।
- यह तय करना कि किन मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत होंगे।
- न्यायालय और पक्षकारों दोनों का समय बचाना।
Issues के बिना मुकदमा स्पष्ट दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता।
15. Ex Parte Decree क्या है?
जब प्रतिवादी मुकदमे में उपस्थित नहीं होता और न्यायालय वादी के पक्ष में एकतरफा निर्णय देता है, तो उसे Ex Parte Decree कहते हैं।
Order IX CPC में इसके प्रावधान हैं।
प्रतिवादी को यह अधिकार है कि वह उचित कारण बताते हुए Ex Parte Decree को निरस्त (Set Aside) करने के लिए आवेदन कर सकता है।
16. Summons (Order V) क्या है?
Summons वह आदेश है, जिसे अदालत प्रतिवादी या गवाह को मुकदमे में उपस्थित होने हेतु भेजती है। इसका उद्देश्य न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है।
Summons की मुख्य बातें:
- इसमें पक्षकार का नाम, मुकदमे का विवरण और तारीख होती है।
- इसे व्यक्तिगत रूप से या डाक/कूरियर/ईमेल से भी भेजा जा सकता है।
2002 संशोधन के बाद Summons की प्रक्रिया सरल की गई है ताकि मामलों में देरी न हो।
17. Decree की परिभाषा और प्रकार बताइए।
धारा 2(2) CPC के अनुसार, Decree न्यायालय का औपचारिक निर्णय है, जिसमें सभी मुद्दों पर अंतिम निस्तारण किया जाता है।
Decree के प्रकार:
- Preliminary Decree – जब कुछ मुद्दे तय हो जाते हैं लेकिन आगे और कार्यवाही शेष रहती है।
- Final Decree – मुकदमे का अंतिम निर्णय।
- Partly Preliminary & Partly Final Decree – आंशिक रूप से दोनों का मिश्रण।
18. Order XXI CPC का महत्व क्या है?
Order XXI CPC डिक्री के निष्पादन (Execution of Decree) से संबंधित है। डिक्री मिलने के बाद उसका पालन कराना जरूरी होता है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं।
निष्पादन के तरीके:
- संपत्ति की कुर्की और नीलामी।
- वेतन से कटौती।
- संपत्ति पर कब्ज़ा दिलाना।
- कारावास।
इस प्रकार, Order XXI CPC न्याय सुनिश्चित करने का अंतिम चरण है।
19. Review (धारा 114, Order XLVII) क्या है?
Review का अर्थ है – न्यायालय अपने ही आदेश/डिक्री पर पुनः विचार करे।
आधार:
- नया और महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य सामने आना।
- स्पष्ट त्रुटि (Error apparent on face of record)।
- अन्य पर्याप्त कारण।
Review उसी न्यायालय में किया जाता है जिसने निर्णय दिया था।
20. Revision (धारा 115 CPC) क्या है?
Revision उच्च न्यायालय की वह शक्ति है, जिसके अंतर्गत वह निचली अदालत के आदेशों की समीक्षा करता है।
आधार:
- जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक जाकर आदेश दिया हो।
- जब उसने आवश्यक अधिकार का प्रयोग नहीं किया हो।
- जब उसने अधिकार का अनुचित प्रयोग किया हो।
Revision अपील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह केवल विधिक त्रुटियों को सुधारने के लिए होता है।
21. Order VI CPC के अंतर्गत Pleadings क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं?
Pleadings वह लिखित विवरण है जिसमें मुकदमे के पक्षकार अपने-अपने दावे और बचाव न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं। CPC के Order VI में Pleadings से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के Pleadings होते हैं –
- Plaint – वादी का दावा।
- Written Statement – प्रतिवादी का उत्तर।
Pleadings का उद्देश्य:
- मुकदमे की सीमाएँ निर्धारित करना।
- विवादित मुद्दों को स्पष्ट करना।
- पक्षकारों को अपने-अपने दावों की तैयारी का अवसर देना।
- अनावश्यक विलंब और अस्पष्टता को समाप्त करना।
नियम यह है कि Pleadings केवल वे तथ्य बताएँगे जिन पर पक्षकार निर्भर करता है, न कि उनके प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि Pleadings का मकसद मुकदमे को सुसंगठित और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना है। यदि Pleadings में आवश्यक तथ्य नहीं दिए गए, तो बाद में उस पर बहस नहीं की जा सकती।
22. Order VII CPC के अंतर्गत Plaint की अस्वीकृति (Rejection of Plaint) कब होती है?
Order VII Rule 11 CPC में Plaint की अस्वीकृति के आधार बताए गए हैं।
मुख्य आधार:
- यदि Plaint से यह स्पष्ट हो कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं है।
- यदि कारण-ए-दावा (Cause of Action) स्पष्ट नहीं किया गया।
- यदि Plaint अपर्याप्त कोर्ट फीस के साथ दाखिल की गई हो और समय पर फीस जमा न की जाए।
- यदि मुकदमा ऐसे न्यायालय में दाखिल किया गया हो जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- यदि Plaint किसी कानून द्वारा वर्जित हो।
महत्व: यह प्रावधान न्यायालय को निरर्थक और झूठे मुकदमों से बचाता है। इससे समय और संसाधन बचते हैं। केस: T. Arivandandam v. T.V. Satyapal (1977) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मुकदमों में कोई वास्तविक कारण-ए-दावा न हो, उन्हें आरंभिक चरण में ही अस्वीकृत कर देना चाहिए।
23. Order IX CPC के अंतर्गत उपस्थिति न होने पर क्या परिणाम होते हैं?
Order IX CPC मुकदमे में पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति से संबंधित है।
- वादी अनुपस्थित हो और प्रतिवादी उपस्थित हो – मुकदमा खारिज (Dismiss) किया जा सकता है।
- दोनों पक्ष अनुपस्थित हों – मुकदमा खारिज हो जाएगा।
- प्रतिवादी अनुपस्थित हो और वादी उपस्थित हो – अदालत एकतरफा (Ex Parte) डिक्री दे सकती है।
- वादी अनुपस्थित हो लेकिन प्रतिवादी मुकदमा स्वीकार कर ले – अदालत प्रतिवादी के पक्ष में आदेश दे सकती है।
Remedy: अनुपस्थित पक्ष उचित कारण बताकर डिक्री या आदेश को निरस्त कराने हेतु आवेदन कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि मुकदमे समय पर चलें और पक्षकार लापरवाही न बरतें।
24. Order XVI CPC के अंतर्गत गवाहों की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाती है?
Order XVI CPC गवाहों की उपस्थिति और उन्हें बुलाने की प्रक्रिया बताता है।
- न्यायालय गवाह को Summons भेजकर बुलाता है।
- गवाह के लिए यात्रा व खर्च (Diet Money) वादी/प्रतिवादी को जमा करना पड़ता है।
- यदि गवाह बिना कारण अनुपस्थित रहता है, तो अदालत उसके विरुद्ध बेंच वारंट जारी कर सकती है।
- गवाह अदालत में उपस्थित होकर साक्ष्य देता है और जिरह (Cross Examination) के लिए उपलब्ध होता है।
महत्व: गवाहों की उपस्थिति मुकदमे की सच्चाई उजागर करने में सहायक होती है। CPC यह सुनिश्चित करता है कि गवाहों की अनुपस्थिति के कारण न्याय में देरी न हो।
25. Order XVIII CPC के अंतर्गत गवाहों की जिरह (Examination of Witnesses) की प्रक्रिया क्या है?
Order XVIII CPC में गवाहों की जिरह (Examination) का प्रावधान है। गवाहों को न्यायालय में तीन प्रकार से परखा जाता है:
- Examination-in-Chief – पक्षकार अपने गवाह से प्रश्न पूछकर साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
- Cross Examination – विपक्षी पक्ष गवाह से जिरह करता है ताकि सच्चाई सामने आए।
- Re-Examination – यदि आवश्यक हो तो मूल पक्षकार फिर से कुछ प्रश्न पूछ सकता है।
2002 संशोधन के बाद गवाहों का मुख्य साक्ष्य लिखित रूप में हलफनामा (Affidavit) के रूप में दाखिल किया जाता है। इससे समय की बचत होती है। यह प्रक्रिया मुकदमे के निष्पक्ष निपटान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
26. Order XX CPC के अंतर्गत डिक्री और निर्णय का क्या महत्व है?
Order XX CPC में निर्णय (Judgment) और डिक्री (Decree) के प्रावधान दिए गए हैं।
- Judgment: न्यायालय द्वारा दिए गए कारण और आधार।
- Decree: Judgment पर आधारित अंतिम आदेश, जिसमें अधिकार और दायित्व तय होते हैं।
निर्णय लिखित होना चाहिए और उसमें स्पष्ट कारण होने चाहिए। अदालत को निर्णय सुनाते समय यह बताना होता है कि किन साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आदेश दिया गया है। डिक्री वही है जो न्यायालय का औपचारिक निष्कर्ष है। इन दोनों का महत्व यह है कि ये मुकदमे की अंतिम परिणति होते हैं और इन्हीं के आधार पर अपील, पुनरीक्षण या निष्पादन की प्रक्रिया चलती है।
27. Order XXXII CPC में नाबालिगों और अस्वस्थ व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान क्या हैं?
Order XXXII CPC में नाबालिग (Minor) और मानसिक रूप से अस्वस्थ (Lunatic) व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
- नाबालिग सीधे मुकदमा दायर नहीं कर सकता और न ही प्रतिवादी के रूप में मुकदमे का संचालन कर सकता है।
- उसके लिए Next Friend या Guardian ad Litem नियुक्त किया जाता है।
- अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी अभिभावक नियुक्त किया जाता है।
उद्देश्य: कमजोर वर्ग के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में संरक्षण देना ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें।
28. Order XXXIX CPC में अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunctions) के प्रावधान क्या हैं?
Order XXXIX CPC में अदालत को यह शक्ति दी गई है कि वह मुकदमे की लंबित स्थिति में किसी पक्ष को किसी कार्य से रोक दे।
आधार:
- यदि मुकदमे का Prima Facie (प्रथम दृष्टया) मामला मजबूत है।
- यदि अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।
- यदि संतुलन (Balance of Convenience) वादी के पक्ष में है।
उदाहरण: संपत्ति विवाद में अदालत प्रतिवादी को संपत्ति बेचने या उसमें निर्माण करने से रोक सकती है।
महत्व: यह प्रावधान मुकदमे के अंतिम निर्णय तक न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होता है।
29. Execution of Decrees (Order XXI CPC) की प्रक्रिया क्या है?
Order XXI CPC डिक्री के निष्पादन से संबंधित है। डिक्री मिलने के बाद उसका पालन कराना आवश्यक है।
निष्पादन के तरीके:
- संपत्ति की कुर्की और नीलामी।
- वेतन या आय से कटौती।
- संपत्ति पर कब्ज़ा दिलाना।
- कारावास (यदि आवश्यक हो)।
महत्व: बिना निष्पादन के डिक्री का कोई मूल्य नहीं है। यह न्याय को व्यावहारिक रूप से लागू करने का साधन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय केवल डिक्री देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे लागू कराना भी उसकी जिम्मेदारी है।
30. CPC में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का महत्व समझाइए।
धारा 89 CPC न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह विवादों को वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR) में भेज सके। इसमें Arbitration, Conciliation, Mediation और Lok Adalat शामिल हैं।
महत्व:
- न्यायालयों पर भार कम करना।
- पक्षकारों को त्वरित और सस्ता न्याय देना।
- आपसी रिश्तों में सुधार लाना।
- छोटे विवादों को शीघ्रता से समाप्त करना।
केस: Salem Advocate Bar Association v. Union of India (2003) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 89 CPC को वैध और न्यायहितकारी माना।