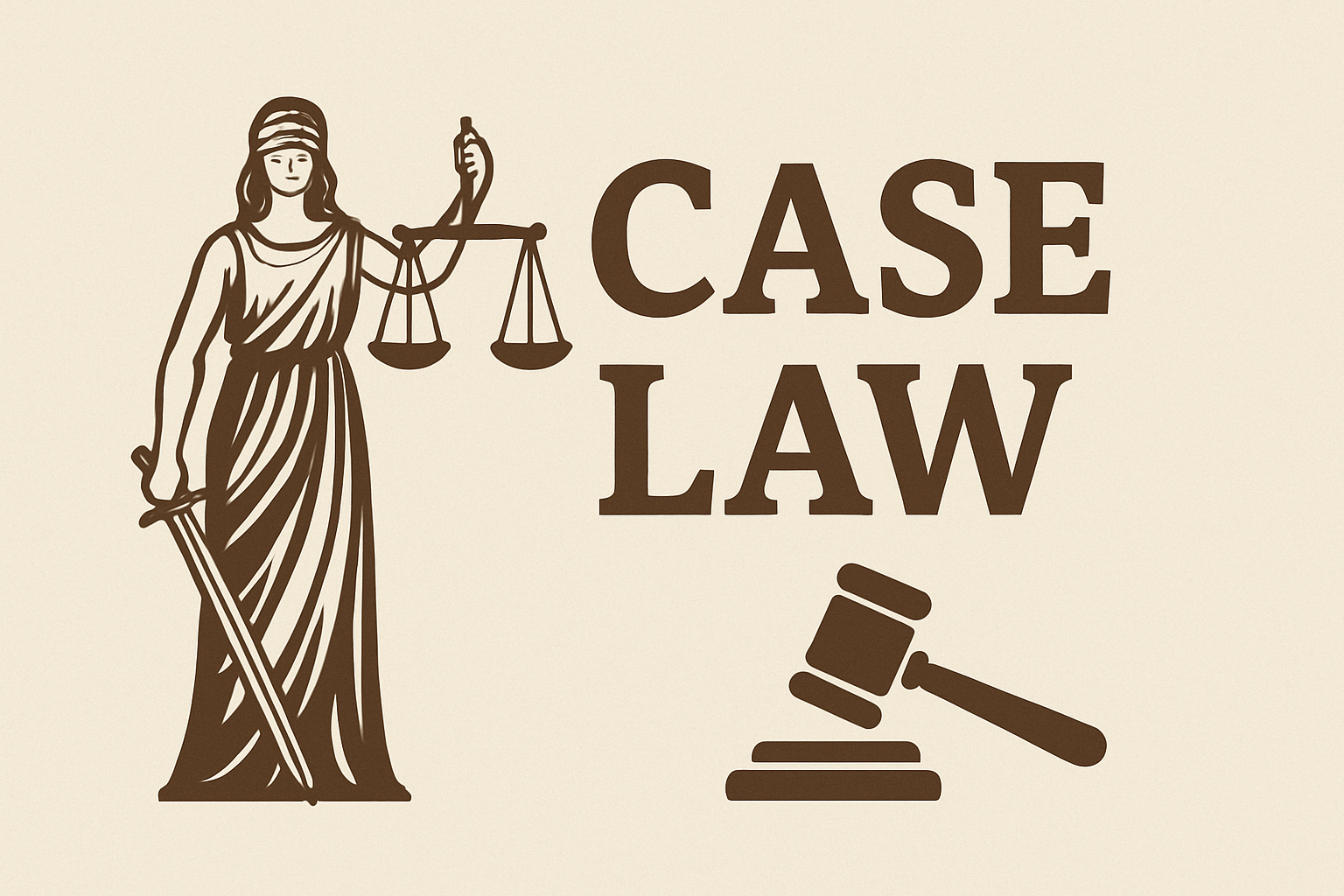“Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation (2015): सुप्रीम कोर्ट ने कहा – CEO या Director को केवल उनके पद के आधार पर आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता”
परिचय
भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं के कार्यों के लिए उनके उच्च अधिकारियों—जैसे चेयरमैन, निदेशक (Director), या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)—की आपराधिक जवाबदेही (Criminal Liability) का प्रश्न लंबे समय से न्यायालयों के विचाराधीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने Sunil Bharti Mittal v. Central Bureau of Investigation (2015) 4 SCC 609 में इस प्रश्न पर निर्णायक टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी कंपनी के अधिकारी या निदेशक को केवल उनके पद या पदनाम के आधार पर आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक उनके विरुद्ध यह स्पष्ट रूप से आरोप न हो कि वे अपराध के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं या उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है।
यह निर्णय न केवल कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व (Corporate Criminal Liability) की सीमाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपराधिक कानून का प्रयोग मनमाने ढंग से न किया जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2G Spectrum Allocation Scam से संबंधित था — जो भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जाता है।
सन 2000 के दशक में, टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस वितरण के दौरान कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ था। इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की, और उसने कई कंपनियों एवं उनके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए।
इस संदर्भ में, Sunil Bharti Mittal, जो उस समय Bharti Cellular Ltd. (अब Bharti Airtel Ltd.) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे, को भी आरोपी बनाया गया।
CBI ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए नीतिगत निर्णयों में हेरफेर किया गया।
हालांकि, सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट (Charge Sheet) में Sunil Bharti Mittal का नाम सीधे तौर पर किसी अपराधी कृत्य में नहीं था। चार्जशीट में मुख्य रूप से कंपनी और कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।
फिर भी, विशेष न्यायाधीश (Special Judge) ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए Sunil Bharti Mittal को व्यक्तिगत रूप से समन (Summon) जारी कर दिया, यह कहते हुए कि कंपनी के कार्यों के लिए उसके प्रमुख (Chairman-cum-Managing Director) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
मुख्य कानूनी प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय थे:
- क्या किसी कंपनी के चेयरमैन या प्रबंध निदेशक को केवल उनके पद के आधार पर आपराधिक कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है?
- क्या आपराधिक न्यायालय को अधिकार है कि वह चार्जशीट में नाम न होने पर भी किसी व्यक्ति को आरोपी बना दे?
- क्या कंपनी के अपराध के लिए उसके अधिकारियों को स्वतः (Vicariously) जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यदि कोई विशेष वैधानिक प्रावधान न हो?
दोनों पक्षों के तर्क
CBI का तर्क:
- Sunil Bharti Mittal कंपनी के प्रमुख हैं और कंपनी के सभी कार्यों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।
- कंपनी ने जिन अपराधों को अंजाम दिया, वे उन्हीं के निर्देश पर हुए।
- इसलिए, उन्हें कंपनी के साथ-साथ आरोपी बनाया जाना चाहिए।
Sunil Bharti Mittal का तर्क:
- चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और न ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि वे किसी अवैध कृत्य में शामिल थे।
- किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता कि वह कंपनी का CEO या Chairman है।
- Vicarious Liability (पर-प्रत्यक्ष दायित्व) आपराधिक मामलों में तभी लागू होती है जब विधि में स्पष्ट प्रावधान हो।
- यह कार्यवाही कानून के विपरीत है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ — न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ — ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि कंपनी और उसके अधिकारियों के बीच कोई स्वचालित आपराधिक जिम्मेदारी का संबंध नहीं होता।
मुख्य निष्कर्ष:
- कंपनी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है।
कंपनी के कार्यों के लिए वही स्वयं जिम्मेदार है। उसके निदेशक या अधिकारी केवल तभी दंडित किए जा सकते हैं जब यह सिद्ध हो कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपराध में भाग लिया या अपराध का आदेश दिया। - चार्जशीट में नाम न होने पर समन जारी नहीं किया जा सकता।
यदि किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट में नहीं है, तो न्यायालय बिना नए साक्ष्य या पर्याप्त कारण के उसे आरोपी नहीं बना सकता। - पद के आधार पर दायित्व अस्वीकार्य है।
केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति कंपनी का CEO, MD या Director है, अपने आप में आपराधिक दायित्व का आधार नहीं बन सकता। - Vicarious Liability का सिद्धांत सीमित है।
सामान्य आपराधिक कानून में vicarious liability लागू नहीं होती जब तक कि किसी विशेष अधिनियम (जैसे Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 141) में स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन
“It is a settled principle of law that there is no vicarious liability in criminal law unless the statute specifically provides so.”
अदालत ने आगे कहा:
“Merely because a person holds a high position in a company or is in charge of its affairs, he does not become liable for the offences committed by the company unless there is sufficient material to show his active role and criminal intent.”
इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने Sunil Bharti Mittal के खिलाफ जारी समन को रद्द (quash) कर दिया।
निर्णय के कानूनी सिद्धांत
- कॉर्पोरेट अलगाव (Corporate Separateness):
कंपनी एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है। उसके अपराधों के लिए उसके अधिकारी स्वतः जिम्मेदार नहीं माने जा सकते। - Mens Rea का महत्व:
आपराधिक दायित्व तभी ठहराया जा सकता है जब व्यक्ति का mens rea (अपराध करने की मंशा या जानकारी) सिद्ध हो। - न्यायिक विवेक का सीमित प्रयोग:
न्यायालय चार्जशीट के बाहर जाकर किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बना सकता, जब तक उसके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य या ठोस कारण न हो। - विधिक प्रावधान की आवश्यकता:
केवल विशेष अधिनियमों में (जैसे Negotiable Instruments Act, Essential Commodities Act) vicarious liability की अनुमति है। सामान्य आपराधिक कानून में यह स्वीकृत नहीं।
निर्णय के प्रभाव
(1) कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्पष्टता:
अब यह स्थापित हो गया कि किसी कंपनी के उच्च अधिकारी को केवल उनके पद के कारण आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता। इससे प्रबंधन में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ा।
(2) अभियोजन एजेंसियों के लिए दिशा:
CBI या अन्य एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी व्यक्ति को तभी आरोपी बनाएं जब उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य हों।
(3) न्यायालयों के लिए मार्गदर्शन:
निचली अदालतें अब यह ध्यान रखेंगी कि वे बिना पर्याप्त आधार के किसी व्यक्ति को अभियुक्त न बनाएं।
(4) Ease of Doing Business में सुधार:
इस निर्णय से कॉर्पोरेट जगत में विश्वास उत्पन्न हुआ कि कानून उन्हें अनावश्यक आपराधिक अभियोजन से बचाएगा।
संबंधित प्रमुख मामलों का उल्लेख
- S.M.S. Pharmaceuticals Ltd. v. Neeta Bhalla (2005) 8 SCC 89
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निदेशक या प्रबंध निदेशक को तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब उनकी व्यक्तिगत भूमिका और संलिप्तता सिद्ध हो। - Maksud Saiyed v. State of Gujarat (2008) 5 SCC 668
– अदालत ने कहा कि कंपनी के अपराध के लिए उसके निदेशकों को तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह दिखाया न जाए कि उन्होंने अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई। - Shiv Kumar Jatia v. State (2019) 17 SCC 193
– इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि कंपनी के MD या Director को केवल पद के आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता।
न्यायालय की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को चेताया कि बिना कारण किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना कानून के शासन (Rule of Law) के विरुद्ध है।
“Courts must be circumspect and judicious while summoning individuals in a criminal case. A mechanical approach would lead to miscarriage of justice.”
निर्णय का सारांश
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मामला | Sunil Bharti Mittal v. CBI (2015) 4 SCC 609 |
| न्यायालय | सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) |
| मुख्य प्रश्न | क्या CEO/Director को केवल पद के आधार पर आरोपी बनाया जा सकता है? |
| निर्णय | नहीं, जब तक प्रत्यक्ष संलिप्तता या अपराध में भूमिका न हो। |
| परिणाम | Sunil Bharti Mittal के खिलाफ समन रद्द। |
| महत्व | Corporate officers को मनमाने आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा। |
महत्वपूर्ण उद्धरण (Key Quote)
“The principle of vicarious liability does not apply to criminal law in the absence of a specific statutory provision.”
— Justice R.M. Lodha, Supreme Court of India (2015)
विश्लेषणात्मक टिप्पणी
इस निर्णय ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कॉर्पोरेट जवाबदेही की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है।
यह बताता है कि “Corporate criminal liability” और “Individual criminal liability” दो भिन्न अवधारणाएँ हैं।
यदि कोई कंपनी किसी अपराध में शामिल है, तो उसके जिम्मेदार अधिकारियों को तभी दंडित किया जा सकता है जब:
- उन्होंने अपराध के आदेश दिए हों;
- उन्होंने अपराध के लिए सक्रिय रूप से सहयोग किया हो; या
- उन्होंने जानबूझकर अपराध की अनुमति दी हो।
केवल पद या अधिकारिक स्थिति (जैसे CEO, MD, Director) का होना, mens rea और actus reus (अपराध का मानसिक और भौतिक तत्व) सिद्ध नहीं करता।
निष्कर्ष
Sunil Bharti Mittal v. CBI (2015) का निर्णय भारतीय न्यायपालिका की उस संतुलित सोच को दर्शाता है जिसमें एक ओर कानून का शासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक नेताओं को अनावश्यक आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा दी जाती है।
यह निर्णय स्पष्ट करता है कि—
- आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत कृत्य पर आधारित है, पद पर नहीं।
- कॉर्पोरेट पदाधिकारी तभी जिम्मेदार हैं जब अपराध में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका सिद्ध हो।
- कानून का उद्देश्य दंड देना है, उत्पीड़न नहीं।
यह फैसला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, न्यायिक विवेक और निष्पक्षता — तीनों के बीच संतुलन स्थापित करता है, और भारतीय कॉर्पोरेट कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।