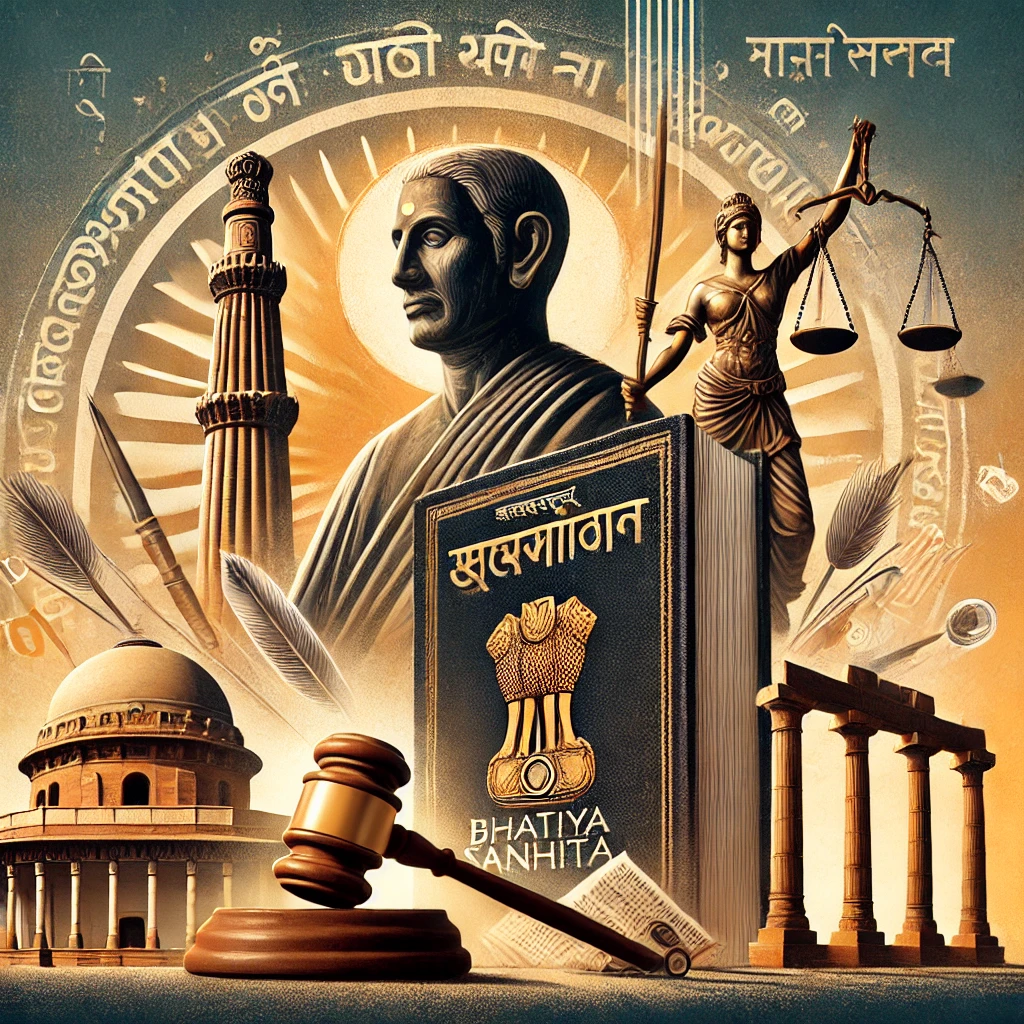📘भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान–LLB विद्यार्थियों हेतु विस्तृत नोट्स
भारतीय संविधान (Indian Constitution) विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि आज इसमें 450 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है और प्रत्येक विधि विद्यार्थी (LLB Student) के लिए इसके मूल प्रावधानों की गहन समझ अनिवार्य है।
1. संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- लिखित और विस्तृत संविधान – यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- संघात्मक व्यवस्था (Federal Structure) – केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन।
- संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) – इंग्लैंड से प्रभावित।
- मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य – नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषा।
- स्वतंत्र न्यायपालिका – संविधान की संरक्षक।
- संविधान की सर्वोच्चता – संसद और कार्यपालिका, दोनों संविधान के अधीन हैं।
- मिश्रित प्रकृति – संघीय ढांचे के साथ-साथ एकात्मक (Unitary) प्रवृत्तियाँ।
2. प्रस्तावना (Preamble)
- प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
- इसमें राज्य की प्रकृति: संप्रभु (Sovereign), समाजवादी (Socialist), पंथनिरपेक्ष (Secular), लोकतांत्रिक (Democratic) और गणराज्य (Republic) बताई गई है।
- लक्ष्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता (Justice, Liberty, Equality, Fraternity)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला (1973) में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
3. नागरिकता (Citizenship) – अनुच्छेद 5 से 11
- संविधान केवल प्रारंभिक नागरिकता को परिभाषित करता है।
- नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का अधिकार संसद को दिया गया है।
- इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।
- नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – अनुच्छेद 12 से 35
मौलिक अधिकार नागरिकों को लोकतंत्र में स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन की गारंटी देते हैं।
- अनुच्छेद 14–18 : समानता का अधिकार (Equality before Law, Untouchability का उन्मूलन, उपाधियों का अंत)।
- अनुच्छेद 19–22 : स्वतंत्रता का अधिकार (भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, यात्रा, व्यवसाय; तथा जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा)।
- अनुच्छेद 23–24 : शोषण के विरुद्ध अधिकार (बाल श्रम पर प्रतिबंध, मानव तस्करी पर रोक)।
- अनुच्छेद 25–28 : धार्मिक स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 29–30 : सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अल्पसंख्यकों की सुरक्षा)।
- अनुच्छेद 32 : संवैधानिक उपचार का अधिकार – डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान की “हृदय और आत्मा” कहा।
5. राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) – अनुच्छेद 36 से 51
- DPSP को आयरलैंड से लिया गया।
- ये राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।
- अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- अनुच्छेद 39 – समान वेतन, श्रमिक व बच्चों की सुरक्षा।
- अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतें।
- अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता।
- अनुच्छेद 45 – 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
- अनुच्छेद 47 – पोषण स्तर सुधार, नशाबंदी।
6. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) – अनुच्छेद 51A
- 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए।
- प्रारंभ में 10, बाद में 86वें संशोधन से 11 कर्तव्य हो गए।
- इनमें संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा प्रदान करना आदि शामिल हैं।
7. केंद्र-राज्य संबंध
- अनुच्छेद 245–263 में विभाजन।
- अनुच्छेद 246 – तीन सूचियां (Union, State, Concurrent)।
- अनुच्छेद 256 – राज्यों का दायित्व कि वे केंद्र के आदेशों का पालन करें।
- वित्तीय संबंधों के लिए अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग।
8. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 52–62 – राष्ट्रपति का चुनाव, योग्यता, कार्यकाल, इत्यादि।
- राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद करता है।
- अनुच्छेद 63–71 – उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति।
9. संसद (Parliament) – अनुच्छेद 79–122
- संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा।
- अनुच्छेद 110 – धन विधेयक।
- अनुच्छेद 111 – राष्ट्रपति की सहमति।
- अनुच्छेद 123 – अध्यादेश की शक्ति।
- संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है।
10. न्यायपालिका
- अनुच्छेद 124–147 – सर्वोच्च न्यायालय।
- अनुच्छेद 214–231 – उच्च न्यायालय।
- अनुच्छेद 32 और 226 – रिट जारी करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 136 – विशेष अनुमति याचिका (SLP)।
- न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और संरक्षक है।
11. संघीय ढांचा
- अनुच्छेद 245–263 – विधायी शक्तियों का विभाजन।
- अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग।
- अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFS)।
- संघीय ढांचे में केंद्र को प्रमुखता प्राप्त है।
12. आपातकालीन प्रावधान – अनुच्छेद 352–360
- अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह)।
- अनुच्छेद 356 – राष्ट्रपति शासन (State Emergency)।
- अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल।
- 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण उदाहरण है।
13. संविधान संशोधन – अनुच्छेद 368
- संसद को संविधान संशोधन का अधिकार।
- साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति – तीन प्रकार की प्रक्रिया।
- केशवानंद भारती मामला (1973) – संसद संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
14. अनुसूचियां
- संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
- प्रथम अनुसूची – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची।
- सातवीं अनुसूची – संघ, राज्य और समवर्ती सूची।
- नवमी अनुसूची – भूमि सुधार संबंधी कानून।
- बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाओं के विषय।
15. अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग।
- अनुच्छेद 324 – निर्वाचन आयोग।
- अनुच्छेद 338 – अनुसूचित जाति आयोग।
- अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (अब निरस्त, 2019)।
- अनुच्छेद 371–371J – विशेष प्रावधान कुछ राज्यों हेतु।
16. न्यायिक निर्णय और संविधान
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) – मूल संरचना सिद्धांत।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) – अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या।
- इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) – लोकतांत्रिक संरचना।
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) – संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती (बाद में संशोधन द्वारा बदला गया)।
🎯 निष्कर्ष
भारतीय संविधान केवल कानून का दस्तावेज़ नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मा को भी दर्शाता है। LLB विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रमुख अनुच्छेदों को न केवल याद रखे बल्कि उनके व्यावहारिक महत्व को भी समझे।
- मौलिक अधिकार लोकतंत्र की सुरक्षा करते हैं।
- DPSP राज्य को सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
- मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं।
- न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्च व्याख्याता है।
संविधान को समझना विधि शिक्षा का आधार है और न्यायिक सेवा जैसी परीक्षाओं में सफलता का सबसे बड़ा साधन भी।
1. प्रस्तावना का महत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें राज्य के स्वरूप और उसके आदर्शों को स्पष्ट किया गया है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बताया गया है। साथ ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे उद्देश्यों की गारंटी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला (1973) में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और यह उसकी मूल संरचना को व्यक्त करती है।
2. मौलिक अधिकारों की भूमिका
मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35) भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। इसमें समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22), शोषण से मुक्ति (अनुच्छेद 23–24), धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28), सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30) तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की “आत्मा” कहा।
3. राज्य के नीति निदेशक तत्व
राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) अनुच्छेद 36–51 में दिए गए हैं। ये राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसमें आर्थिक समानता, ग्राम पंचायतों की स्थापना, समान नागरिक संहिता, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर सुधार आदि के प्रावधान हैं। यद्यपि DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन ये राज्य की नीतियों के संचालन में मूलभूत दिशा प्रदान करते हैं।
4. मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में निहित हैं। इन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया और वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। इसमें संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, महिलाओं का सम्मान और बच्चों को शिक्षा दिलाना शामिल है। ये नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं।
5. संघीय ढांचा
भारतीय संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है लेकिन इसमें केंद्र की प्रधानता स्पष्ट है। अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र महत्वपूर्ण विषयों जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा पर कानून बनाता है, जबकि राज्य स्थानीय विषयों पर। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। इस प्रकार भारत को “संघात्मक व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र” वाला राज्य कहा जाता है।
6. राष्ट्रपति की भूमिका
राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और अधिकार दिए गए हैं। उनका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। वे कार्यपालिका की सभी शक्तियों के धारक हैं लेकिन वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद करती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यद्यपि उनकी भूमिका औपचारिक है, फिर भी आपातकालीन प्रावधानों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
7. संसद की शक्तियाँ
संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की सहमति, तथा अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है। संसद कानून बनाने, वित्तीय नियंत्रण, सरकार पर निगरानी और संविधान संशोधन जैसे कार्य करती है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल स्तंभ है।
8. न्यायपालिका की भूमिका
भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और शक्तिशाली है। अनुच्छेद 124–147 में सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214–231 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट दाखिल कर सकते हैं। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और व्याख्याता है तथा यह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है। केशवानंद भारती मामला ने इसे मूल संरचना की रक्षा का दायित्व भी सौंपा।
9. आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद 352–360 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल (352), राष्ट्रपति शासन (356) और वित्तीय आपातकाल (360) में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। 1975–77 का आपातकाल इसका प्रमुख उदाहरण है जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। इन प्रावधानों से भारत की एकात्मक प्रवृत्ति सामने आती है।
10. संविधान संशोधन
संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। संसद साधारण, विशेष और विशेष + राज्यों की सहमति से संशोधन कर सकती है। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। केशवानंद भारती मामला (1973) ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसद संविधान की “मूल संरचना” को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत भारतीय संविधान को स्थायित्व और लचीलापन दोनों प्रदान करता है।
11. अनुच्छेद 14 का महत्व
अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का सबसे मूलभूत प्रावधान है, जो “समानता के अधिकार” की गारंटी देता है। इसमें दो बातें शामिल हैं – (1) Equality before Law अर्थात सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर हैं, और (2) Equal Protection of Laws अर्थात समान परिस्थितियों में सभी को समान संरक्षण मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी को एक जैसा व्यवहार मिलेगा, बल्कि यह है कि भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवस्था हो सकती है, बशर्ते वह तार्किक आधार पर हो। न्यायालय ने कई मामलों में कहा कि अनुच्छेद 14 भेदभाव नहीं बल्कि “तार्किक वर्गीकरण” (Reasonable Classification) की अनुमति देता है।
12. अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है – (1) वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (2) सभा की स्वतंत्रता, (3) संगठन बनाने की स्वतंत्रता, (4) आवागमन की स्वतंत्रता, (5) निवास की स्वतंत्रता, और (6) व्यवसाय/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएँ पूर्ण नहीं हैं, बल्कि राज्य “जनहित” के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
13. अनुच्छेद 21 का व्यापक महत्व
अनुच्छेद 21 कहता है – “किसी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।” प्रारंभ में इसका अर्थ सीमित था, परंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” उचित, न्यायपूर्ण और युक्तिसंगत होनी चाहिए। आज अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निजता और गरिमा से जीने का अधिकार भी शामिल है।
14. अनुच्छेद 32 की भूमिका
अनुच्छेद 32 को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की “हृदय और आत्मा” कहा। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है जब उसका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो। सर्वोच्च न्यायालय इस स्थिति में रिट जारी करता है – हेबियस कॉर्पस, मण्डमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी। इस प्रावधान से नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रत्यक्ष साधन मिलता है।
15. अनुच्छेद 226 और उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी रिट जारी कर सके। यह अनुच्छेद 32 से व्यापक है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों से परे अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। इस कारण उच्च न्यायालय नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी विकल्प है।
16. समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है, जो कहता है कि राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक जैसे व्यक्तिगत विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हों। यह धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है, लेकिन विविध धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे लागू करने में कठिनाई आती रही है।
17. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अनुच्छेद 51A में माता-पिता का यह कर्तव्य जोड़ा गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएँ। यह प्रावधान देश में सार्वभौमिक साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
18. आपातकाल में मौलिक अधिकार
आपातकालीन स्थिति (अनुच्छेद 352) में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 इसके लिए प्रावधान करते हैं। हालांकि, 44वें संशोधन (1978) के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। 1975–77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र में ऐसा उदाहरण है जब प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया।
19. संविधान की मूल संरचना सिद्धांत
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की “मूल संरचना” को नहीं बदल सकती। मूल संरचना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और मौलिक अधिकार शामिल हैं। यह सिद्धांत संविधान को स्थायित्व प्रदान करता है और उसे मनमाने संशोधनों से बचाता है।
20. अनुसूचियों का महत्व
भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (पहली अनुसूची), केंद्र–राज्य शक्तियों का विभाजन (सातवीं अनुसूची), भूमि सुधार संबंधी कानून (नवमी अनुसूची) और नगरपालिकाओं से जुड़े विषय (बारहवीं अनुसूची) शामिल हैं। अनुसूचियां संविधान को व्यवस्थित बनाती हैं और विषयों को श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती हैं।