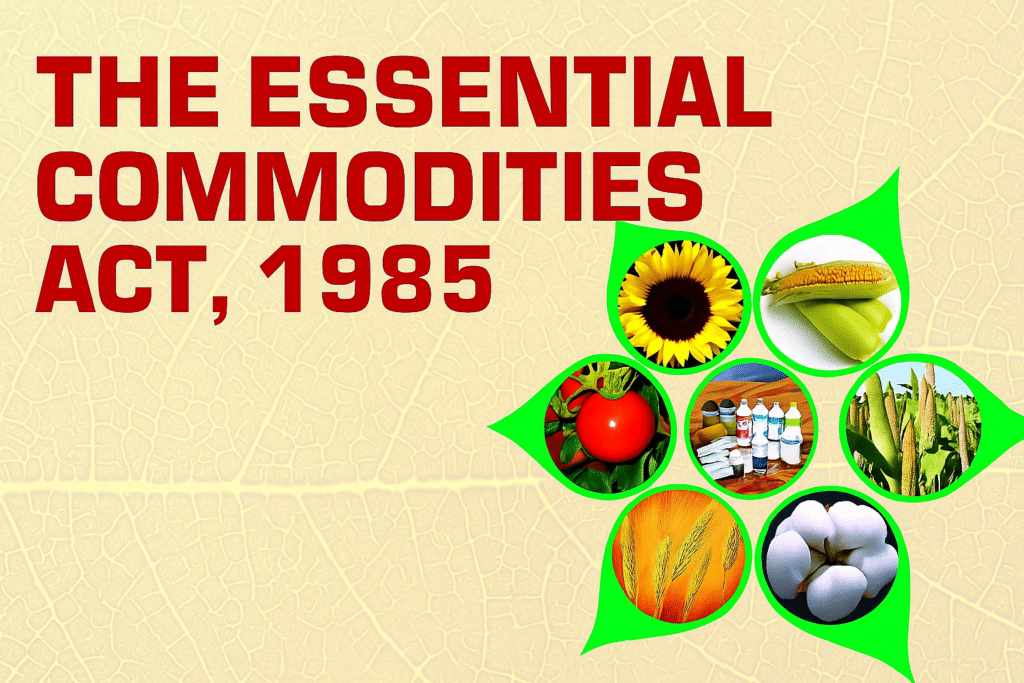आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 (Essential Commodities Act, 1985) : एक विस्तृत अध्ययन
प्रस्तावना
भारत जैसे विशाल और जनसंख्या प्रधान देश में वस्तुओं की उपलब्धता और उनकी उचित कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। विशेष रूप से खाद्यान्न, दवाइयाँ, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य दैनिक जीवन की वस्तुएँ आम नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यदि इन वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो जाए या जमाखोरी और मुनाफाखोरी के कारण इनकी कीमतें अत्यधिक बढ़ जाएँ तो समाज में असंतुलन और असंतोष पैदा हो सकता है। इसी कारण सरकार ने समय-समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू किया ताकि ऐसे संकट की स्थिति से निपटा जा सके।
हालाँकि मूल रूप से यह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, लेकिन 1985 में पुनः इसका व्यापक रूप से संशोधन और पुनर्प्रस्तुतीकरण किया गया। इसलिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 भी कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, जमाखोरी पर रोक लगाना, मुनाफाखोरी को रोकना और उपभोक्ताओं को संरक्षण देना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खाद्यान्न संकट, औद्योगिक कच्चे माल की कमी और आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता एक गंभीर चुनौती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही ब्रिटिश सरकार ने वस्तुओं पर नियंत्रण की व्यवस्था शुरू की थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भी इस प्रणाली को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई।
- 1955 का मूल अधिनियम – संसद ने Essential Commodities Act, 1955 पारित किया, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए कि वह कुछ वस्तुओं को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित कर सके और उनकी आपूर्ति व वितरण पर नियंत्रण रख सके।
- बाद के वर्षों में बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, बढ़ती जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति, तथा उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए 1985 में व्यापक संशोधन किए गए।
- 1985 अधिनियम ने मूल कानून को और अधिक कड़ा तथा प्रभावी बनाया।
उद्देश्य (Objectives of the Act)
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
- आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना – ताकि हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएँ मिल सकें।
- कीमतों पर नियंत्रण रखना – जमाखोरी और कृत्रिम कमी द्वारा कीमतें बढ़ाने पर रोक लगाना।
- वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करना – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीब एवं कमजोर वर्ग को उचित दर पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- मुनाफाखोरी और काला बाज़ारी रोकना – ताकि समाज में आर्थिक असमानता और शोषण की स्थिति न बने।
- उपभोक्ता संरक्षण – आम जनता को राहत और सुविधा प्रदान करना।
प्रमुख प्रावधान (Major Provisions of the Act)
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं जो सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हैं–
1. आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा (Essential Commodities)
इस अधिनियम के अनुसार, सरकार समय-समय पर किसी भी वस्तु को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित कर सकती है। इन वस्तुओं में शामिल हो सकते हैं–
- खाद्यान्न (Rice, Wheat, Pulses)
- दालें और खाद्य तेल
- पेट्रोलियम उत्पाद (Petrol, Diesel, Kerosene, LPG)
- औषधियाँ
- उर्वरक
- चीनी
- अन्य वस्तुएँ जिन्हें सरकार आवश्यक समझे
2. केंद्र सरकार की शक्तियाँ
- उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण।
- स्टॉक की सीमा तय करना।
- मूल्य निर्धारण (Price Fixation)।
- आयात और निर्यात पर प्रतिबंध।
- आवश्यक वस्तुओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना।
3. राज्य सरकार की भूमिका
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी आदेश देने की शक्ति देती है ताकि स्थानीय स्तर पर जमाखोरी और काला बाज़ारी को नियंत्रित किया जा सके।
4. दंडात्मक प्रावधान (Penal Provisions)
- जमाखोरी और काला बाज़ारी करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- दोषी को 3 माह से 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होते हैं।
5. कब्ज़ा और जब्ती (Seizure and Confiscation)
यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति अवैध रूप से आवश्यक वस्तु का भंडारण करता है तो सरकार उसका स्टॉक ज़ब्त कर सकती है और आवश्यकतानुसार PDS के माध्यम से जनता में वितरित कर सकती है।
6. विशेष न्यायालय (Special Courts)
इस अधिनियम के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं।
संशोधन और सुधार
समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए जाते रहे हैं। प्रमुख संशोधन–
- 1976 संशोधन – कठोर दंडात्मक प्रावधान लाए गए।
- 1981 संशोधन – पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों पर विशेष नियंत्रण।
- 1985 संशोधन – मूल अधिनियम को और व्यापक बनाया गया।
- 2002 संशोधन – आवश्यक वस्तुओं की सूची को संकुचित किया गया।
- 2020 संशोधन – कृषि सुधार कानूनों के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें कृषि उपज पर नियंत्रण को सीमित किया गया।
न्यायिक दृष्टिकोण (Judicial Interpretation)
भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर इस अधिनियम की व्याख्या की है।
- State of Rajasthan v. G. Chawla (1959) – सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष शक्तियाँ दी जा सकती हैं।
- Harakchand Ratanchand Banthia v. Union of India (1969) – अदालत ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार का नियंत्रण वैध है।
- Kishan Chand v. State of Haryana (1980) – जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही को उचित ठहराया गया।
प्रशासनिक तंत्र
इस अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है।
- केंद्र सरकार – नीति निर्माण और दिशा-निर्देश जारी करती है।
- राज्य सरकारें – निगरानी, छापे, ज़ब्ती और अभियोजन की कार्यवाही करती हैं।
- विशेष पुलिस बल – जमाखोरी और काला बाज़ारी के विरुद्ध कार्यवाही करता है।
महत्त्व (Significance of the Act)
- यह अधिनियम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करता है।
- गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षा कवच है।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायक।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में उपयोगी।
आलोचना (Criticism of the Act)
यद्यपि इस अधिनियम का उद्देश्य जनहित में है, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएँ की जाती हैं–
- अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप – यह बाजार की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
- भ्रष्टाचार की संभावना – अधिकारियों द्वारा गलत उपयोग की संभावना रहती है।
- व्यापारियों का विरोध – व्यापारी वर्ग इसे अपने व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अंकुश मानता है।
- वस्तुओं की कृत्रिम कमी – कई बार नियंत्रण के कारण बाजार में वस्तुएँ और दुर्लभ हो जाती हैं।
- PDS में भ्रष्टाचार – आवश्यक वस्तुओं के वितरण में गड़बड़ियाँ।
2020 के कृषि सुधारों के संदर्भ में अधिनियम
2020 में सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु तीन प्रमुख कानून बनाए, जिनमें से एक Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 था। इसके तहत–
- कुछ कृषि उपज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया।
- भंडारण की सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू करने का प्रावधान।
- उद्देश्य – कृषि व्यापार को स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बनाना।
हालाँकि किसानों ने इसका विरोध किया और इसे कृषि कानूनों के विरोध का प्रमुख कारण माना गया।
निष्कर्ष
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 भारतीय उपभोक्ता संरक्षण और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण विधिक साधन है। इसने सरकार को यह शक्ति दी है कि वह जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगा सके तथा आम जनता को आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सके।
हालाँकि, समय-समय पर इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस होती रही है ताकि यह बदलते आर्थिक परिवेश के अनुकूल हो सके। आधुनिक उदारीकृत और वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप को संतुलित करना आवश्यक है, लेकिन आम जनता के हित और खाद्यान्न सुरक्षा की रक्षा सर्वोपरि है।
इस प्रकार यह अधिनियम भारतीय विधि प्रणाली में उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है।
10 Short Answers
1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 का उद्देश्य क्या है?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 का मुख्य उद्देश्य देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, कीमतों को स्थिर रखना और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखना है। अधिनियम केंद्र व राज्य सरकार को उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और भंडारण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ काला बाज़ारी और कृत्रिम कमी रोकने में सहायक है।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम में ‘आवश्यक वस्तु’ की परिभाषा क्या है?
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ‘आवश्यक वस्तु’ वह वस्तु है जिसे सरकार समय-समय पर जनता के हित में नियंत्रित करने का निर्णय लेती है। इसमें खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, दाल), खाद्य तेल, दवाएँ, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि शामिल हैं। सरकार इन वस्तुओं की कीमत, भंडारण सीमा, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण कर सकती है ताकि आम जनता तक वस्तु उचित मूल्य पर पहुँच सके और काला बाज़ारी तथा जमाखोरी रोकी जा सके।
3. केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ आवश्यक वस्तु अधिनियम में
केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करती है और उनके उत्पादन, मूल्य निर्धारण, भंडारण व वितरण पर नियंत्रण रख सकती है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत केंद्र के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने क्षेत्रों में जमाखोरी रोकने और वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था करती हैं। दोनों स्तरों की सरकारें आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए आदेश जारी कर सकती हैं, छापे मार सकती हैं और दोषियों के खिलाफ अभियोजन कर सकती हैं।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम में स्टॉक लिमिट का महत्व
स्टॉक लिमिट का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का जमाखोरी रोकना है। यह अधिनियम व्यापारियों, निर्माताओं और वितरकों को सीमित मात्रा से अधिक भंडारण करने से रोकता है। इससे कृत्रिम कमी और काला बाज़ारी की प्रवृत्ति कम होती है। स्टॉक लिमिट लागू करने से वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहती है और कीमतें स्थिर रहती हैं। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाता है।
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी, काला बाज़ारी या स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। दोषी को तीन माह से सात वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय होते हैं और विशेष न्यायालयों में सुनवाई होती है। दंड का उद्देश्य व्यापारियों और वितरकों को अनुशासन में रखना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना है।
6. आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण
आवश्यक वस्तु अधिनियम उपभोक्ताओं को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, दालें, तेल आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हों और जमाखोरी व मुनाफाखोरी से बची रहें। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हित में नियंत्रण आदेश जारी करती हैं। इस प्रकार अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण का एक प्रमुख साधन है जो समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखता है।
7. आवश्यक वस्तु अधिनियम में न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायालयों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के महत्व को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर इसके तहत नियंत्रण के आदेशों को वैध ठहराया है। जैसे State of Rajasthan v. G. Chawla में अदालत ने कहा कि जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायालय इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के हित में एक संवैधानिक साधन मानते हैं।
8. आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
आवश्यक वस्तु अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। प्रमुख संशोधन 1976, 1981, 1985, 2002 और 2020 में हुए। 1985 का संशोधन अधिनियम को व्यापक बनाया। 2020 में कृषि सुधारों के तहत कुछ कृषि उपज को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर किया गया और भंडारण सीमा में बदलाव किया गया। इसका उद्देश्य कृषि व्यापार में स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था।
9. आवश्यक वस्तु अधिनियम के महत्व
आवश्यक वस्तु अधिनियम उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करता है। यह आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जमाखोरी और काला बाज़ारी रोकता है, और कीमतों को स्थिर रखता है। यह गरीब और कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने में सहायक है। देश में खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में यह अधिनियम एक अहम साधन है।
10. आवश्यक वस्तु अधिनियम पर आलोचना
हालांकि आवश्यक वस्तु अधिनियम उपभोक्ताओं के हित में है, परंतु इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि यह अधिनियम बाजार की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। कई बार इसकी वजह से वस्तुओं में कृत्रिम कमी हो जाती है। PDS में भ्रष्टाचार और वितरण में गड़बड़ी भी एक बड़ा मुद्दा है।