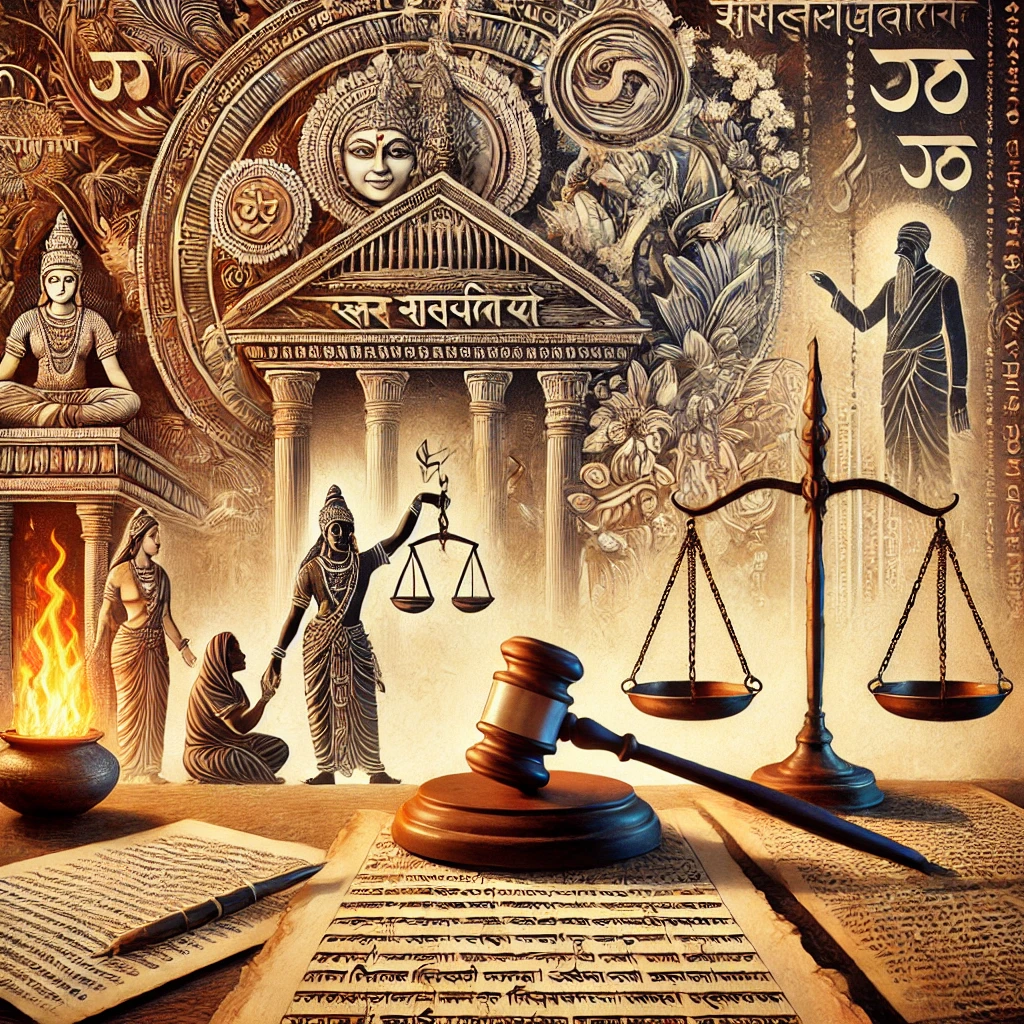हिंदू विवाह अधिनियम और तलाक के आधारः सरल भाषा में
भूमिका
भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह केवल पति-पत्नी के बीच का समझौता नहीं, बल्कि जीवनभर का धार्मिक और सामाजिक बंधन है। लेकिन समय के साथ यह मान्यता भी विकसित हुई कि यदि पति-पत्नी के बीच ऐसा विवाद हो जाए कि साथ रहना असंभव हो जाए, तो विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) बनाया गया।
इस अधिनियम में विवाह की वैधता की शर्तें, पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्य, तथा विवाह विच्छेद (Divorce) के आधार स्पष्ट किए गए हैं। आगे हम इसे सरल भाषा में समझेंगे।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का परिचय
- लागू होने की तिथि: 18 मई, 1955
- लागू क्षेत्र: संपूर्ण भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, हालांकि अब 2019 के बाद वहां भी लागू है)।
- लागू धर्म: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख।
इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदू विवाह को नियमित करना और पति-पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना था। इसमें विवाह की वैधता, विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया, तलाक, भरण-पोषण, संतानों की वैधता और पुनर्विवाह से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
विवाह की शर्तें (Section 5, Hindu Marriage Act)
किसी विवाह को वैध माने जाने के लिए अधिनियम की धारा 5 में कुछ शर्तें दी गई हैं:
- पति-पत्नी दोनों की आयु—पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष।
- विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो।
- दोनों पक्ष मानसिक रूप से सक्षम हों।
- निकट संबंध (Sapinda Relationship) या निषिद्ध संबंध (Prohibited Relationship) में विवाह न हो, जब तक कि प्रथा द्वारा अनुमति न हो।
तलाक का अर्थ
तलाक का मतलब है—पति-पत्नी के बीच विवाह संबंध का कानूनी अंत। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के लिए धारा 13 में आधार दिए गए हैं। पहले यह प्रावधान सीमित था, लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से इसे व्यापक बनाया गया।
तलाक के आधार (Grounds of Divorce)
1. व्यभिचार (Adultery)
यदि पति या पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाते हैं, तो यह तलाक का आधार है।
- उदाहरण: यदि पत्नी को यह पता चले कि पति किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रखता है, तो वह तलाक की याचिका दायर कर सकती है।
- केस लॉ: Subbaramma v. Saraswathi (1964) में अदालत ने कहा कि लगातार या एक बार भी अवैध संबंध तलाक का आधार बन सकता है।
2. क्रूरता (Cruelty)
यदि एक पक्ष दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक अत्याचार करता है, तो यह तलाक का आधार है।
- शारीरिक क्रूरता: मारपीट, शारीरिक चोट।
- मानसिक क्रूरता: अपमान, तिरस्कार, मानसिक यातना।
- केस लॉ: N.G. Dastane v. S. Dastane (1975) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता भी तलाक का आधार है।
3. परित्याग (Desertion)
यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के लगातार कम से कम दो वर्ष तक दूसरे को छोड़कर रहता है, तो तलाक मिल सकता है।
- परित्याग का मतलब है—साथ न रहना और साथ रहने की इच्छा भी न होना।
- केस लॉ: Bipinchandra v. Prabhavati (1957) में परित्याग की परिभाषा दी गई।
4. धर्म परिवर्तन (Conversion)
यदि कोई पक्ष हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो दूसरा पक्ष तलाक की याचिका दायर कर सकता है।
- उदाहरण: पति हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है।
5. मानसिक विकार (Mental Disorder)
यदि पति या पत्नी किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जिससे साथ रहना असंभव हो, तो यह तलाक का आधार है।
- इसमें स्किजोफ्रेनिया, गंभीर अवसाद जैसी स्थितियाँ शामिल हैं।
- केस लॉ: R. Lakshmi Narayan v. Santhi (2001) में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रोग की गंभीरता को तलाक का आधार माना।
6. संक्रामक रोग (Communicable Disease)
यदि पति या पत्नी किसी ऐसे असाध्य और संक्रामक रोग से पीड़ित है, जो यौन संबंध के माध्यम से फैल सकता है, जैसे कुष्ठ रोग या यौन रोग, तो तलाक दिया जा सकता है।
7. संन्यास (Renunciation of World)
यदि पति या पत्नी ने संन्यास ले लिया है और सामाजिक जीवन से अलग हो गया है, तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है।
8. मृत्यु का अनुमान (Presumption of Death)
यदि पति या पत्नी लगातार सात वर्षों तक जीवित होने की सूचना नहीं देता और उसका कोई पता नहीं चलता, तो दूसरा पक्ष उसे मृत मानकर तलाक ले सकता है।
विशेष आधार केवल पत्नी के लिए (Section 13(2))
पत्नी को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं:
- यदि पति के पास दूसरी पत्नी है (विवाह के समय)।
- पति बलात्कार, सोडोमी या बेस्टियालिटी का दोषी हो।
- विवाह के समय पत्नी नाबालिग थी और उसने 15 से 18 वर्ष के बीच विवाह को अस्वीकार कर दिया।
- पति ने दूसरी पत्नी को छोड़ दिया है।
आपसी सहमति से तलाक (Divorce by Mutual Consent) — Section 13B
1976 के संशोधन से यह प्रावधान जोड़ा गया।
- पति-पत्नी दोनों यह साबित करें कि वे कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हैं और भविष्य में साथ रहने की इच्छा नहीं है।
- वे अदालत में संयुक्त याचिका दाखिल करते हैं।
- Cooling-off Period: 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दोनों विचार कर सकें।
- इसके बाद तलाक डिक्री मिल सकती है।
केस लॉ: Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) — सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है, यदि अदालत को लगे कि पुनर्मिलन संभव नहीं है।
तलाक की प्रक्रिया (Procedure of Divorce)
- याचिका दाखिल करना: संबंधित फैमिली कोर्ट या जिला न्यायालय में।
- नोटिस जारी: दूसरे पक्ष को अदालत में बुलाया जाता है।
- सबूत और सुनवाई: दोनों पक्षों के दावे और सबूत सुने जाते हैं।
- निर्णय: यदि अदालत को तलाक के आधार सही लगते हैं, तो डिक्री जारी की जाती है।
तलाक के परिणाम
- पति-पत्नी का वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है।
- दोनों पुनर्विवाह कर सकते हैं।
- पत्नी को भरण-पोषण (Maintenance) का अधिकार मिल सकता है।
- बच्चों की संतान अभिरक्षा (Custody of Children) अदालत तय करती है।
महत्वपूर्ण केस लॉ का सारांश
- Subbaramma v. Saraswathi (1964) — व्यभिचार पर तलाक।
- N.G. Dastane v. S. Dastane (1975) — मानसिक क्रूरता तलाक का आधार।
- Bipinchandra v. Prabhavati (1957) — परित्याग की परिभाषा।
- Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) — आपसी सहमति तलाक में 6 महीने की अवधि लचीली।
- R. Lakshmi Narayan v. Santhi (2001) — मानसिक विकार तलाक का आधार।
निष्कर्ष
हिंदू विवाह अधिनियम ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि विवाह केवल धार्मिक बंधन नहीं है, बल्कि पति-पत्नी दोनों के अधिकार और सम्मान का संतुलन भी है। यदि विवाह असफल हो जाए और साथ रहना असंभव हो, तो तलाक एक वैध और आवश्यक उपाय है।
आज तलाक के आधार आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित हो रहे हैं। अदालतें भी यह मानती हैं कि तलाक को आसान और न्यायपूर्ण बनाना आवश्यक है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
हिंदू विवाह अधिनियम और तलाक के आधार से जुड़े 10 शॉर्ट आंसर
1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 कब लागू हुआ?
→ यह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ।
2. हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें किस धारा में दी गई हैं?
→ धारा 5, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955।
3. बहुविवाह (Polygamy) की स्थिति में विवाह की वैधता क्या है?
→ यदि पति या पत्नी में से कोई जीवित पति/पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो वह विवाह शून्य (Void) होगा।
4. विवाह की न्यूनतम आयु क्या है?
→ पुरुष के लिए 21 वर्ष और स्त्री के लिए 18 वर्ष।
5. शून्य विवाह (Void Marriage) किसे कहते हैं?
→ ऐसा विवाह जो प्रारंभ से ही अमान्य हो, जैसे – बहुविवाह, निषिद्ध संबंध में विवाह।
6. तलाक के सामान्य आधार कितने हैं?
→ धारा 13 में तलाक के 9 मुख्य आधार बताए गए हैं, जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग आदि।
7. व्यभिचार (Adultery) किसे कहा जाता है?
→ जब पति या पत्नी विवाह के दौरान अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो इसे व्यभिचार कहते हैं।
8. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B किससे संबंधित है?
→ पारस्परिक सहमति (Mutual Consent Divorce) से।
9. तलाक के बाद पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार किस धारा में दिया गया है?
→ धारा 25, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955।
10. हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विवाह कब संभव है?
→ जब पति-पत्नी को विधिवत तलाक मिल जाए या साथी की मृत्यु हो जाए।