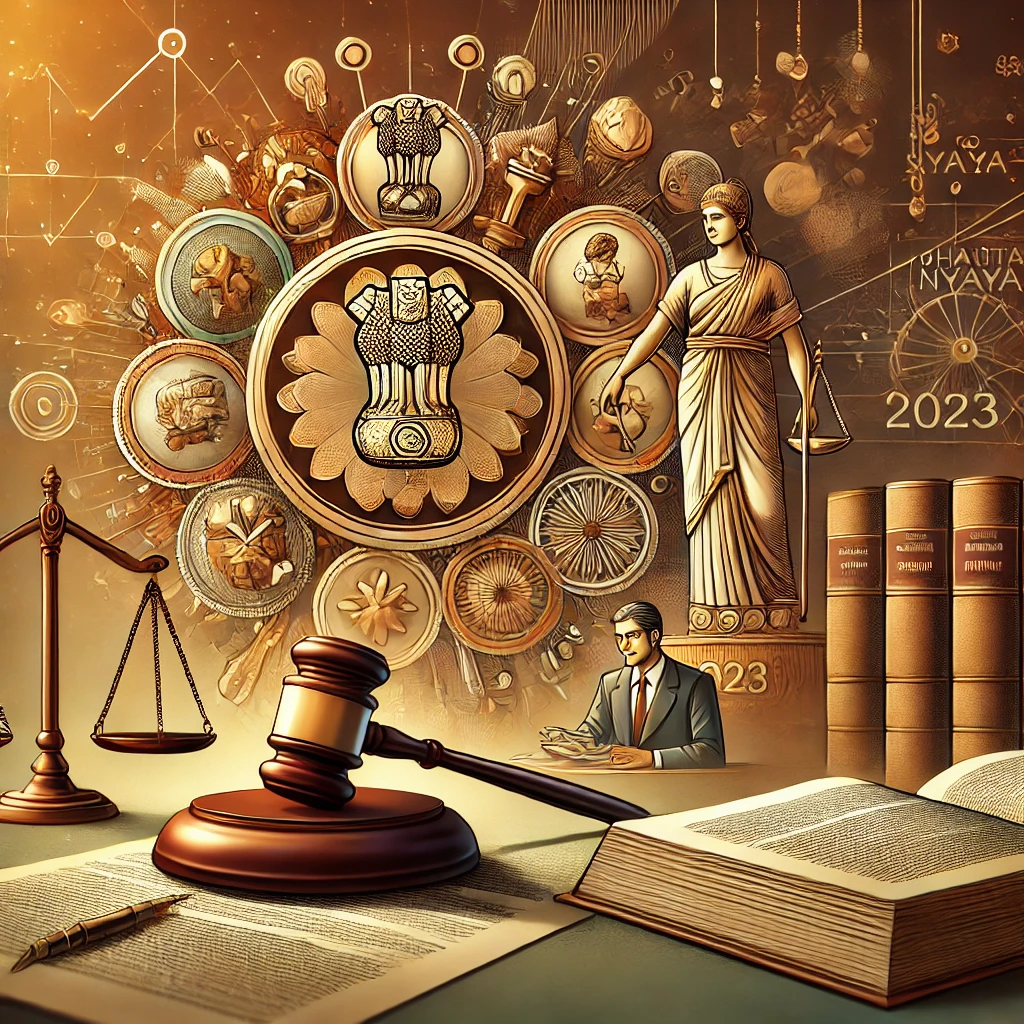बीएनएस धारा 32: धमकी के अधीन किए गए कार्य और आपराधिक दायित्व से मुक्ति
भारत में आपराधिक कानून का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराधियों को दंडित करना और निर्दोषों की रक्षा करना है। परंतु न्यायशास्त्र यह भी मानता है कि हर परिस्थिति में किसी व्यक्ति को समान रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो, जहाँ उसकी तत्काल मृत्यु का खतरा हो और उसी कारणवश वह कोई अपराध करने के लिए बाध्य हो, तो क्या उसे भी वही दंड दिया जाना चाहिए जो एक स्वेच्छा से अपराध करने वाले को दिया जाता है? इसी प्रश्न का समाधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की धारा 32 प्रदान करती है।
1. बीएनएस धारा 32 का विधिक प्रावधान
धारा 32 कहती है कि—
हत्या और राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय हैं, को छोड़कर कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा उस समय इस धमकी के अधीन किया गया हो कि यदि उसने वह कार्य नहीं किया तो उसे तत्काल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि कार्य करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम किसी भय के कारण स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं डाला हो।
2. उद्देश्य और दार्शनिक आधार
धारा 32 का मूल दर्शन यह है कि—
- कानून असंभव को अपेक्षित नहीं कर सकता।
- यदि किसी व्यक्ति के सामने केवल दो विकल्प हों—या तो वह अपराध करे या उसकी तत्काल मृत्यु हो—तो ऐसे में उसका चयन स्वतंत्र इच्छा (free will) से नहीं बल्कि बाध्यता (compulsion) से किया गया माना जाएगा।
- ऐसे मामलों में दंड देना अन्यायपूर्ण और अमानवीय होगा।
यह सिद्धांत प्राचीन रोमन कानून और अंग्रेजी कॉमन लॉ से भी प्रेरित है, जहाँ यह माना गया है कि “कानून व्यक्ति से वही अपेक्षा करता है जो उसकी सामर्थ्य में हो।”
3. आईपीसी और बीएनएस का अंतर
भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 94 में भी यही प्रावधान था। बीएनएस 2023 में इसे लगभग उसी रूप में धारा 32 के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
अंतर यह है कि बीएनएस की भाषा अधिक स्पष्ट और सरल की गई है, जिससे व्यावहारिक अनुप्रयोग में भ्रम न रहे।
4. धारा 32 की प्रमुख विशेषताएँ
- सामान्य अपवाद (General Exception): यह धारा अपराध के सामान्य अपवादों में आती है।
- धमकी का स्वरूप: धमकी इतनी गंभीर होनी चाहिए कि व्यक्ति को तत्काल मृत्यु का भय हो।
- सीमा: हत्या और देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध इसमें शामिल नहीं हैं।
- स्वेच्छा से स्थिति में न आना: यदि व्यक्ति ने स्वयं जानबूझकर अपराधियों के साथ संबंध बनाए हों, तो यह बचाव नहीं मिलेगा।
5. स्पष्टीकरण (Explanations) का महत्व
- स्पष्टीकरण 1: यदि कोई व्यक्ति डकैतों के गिरोह में शामिल हो जाता है और बाद में वे उसे अपराध करने को मजबूर करें, तो उसे धारा 32 का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने स्वेच्छा से खुद को ऐसी स्थिति में डाला।
- स्पष्टीकरण 2: यदि कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और तत्काल मृत्यु की धमकी देकर अपराध कराया जाए, तो उसे यह बचाव उपलब्ध होगा।
ये दोनों स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल वास्तविक मजबूरी वाले मामलों में ही यह धारा लागू हो।
6. न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायालयों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है कि “Compulsion by threat of instant death can absolve criminal liability except in cases of murder and offences against the State punishable with death.”
उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में न्यायालय ने कहा कि—
- यदि किसी व्यक्ति को डकैत पकड़कर धमकी देते हैं कि दरवाज़ा न तोड़ने पर उसे मार देंगे और वह मजबूरी में दरवाज़ा तोड़ देता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।
- परंतु यदि वही व्यक्ति धमकी के कारण हत्या कर देता है, तो उसे इस धारा का संरक्षण नहीं मिलेगा।
7. व्यावहारिक उदाहरण
- लागू होने वाला उदाहरण:
एक लोहार को डकैत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यदि उसने अपने औज़ार से दरवाज़ा नहीं तोड़ा तो उसे तुरंत मार देंगे। लोहार मजबूरी में दरवाज़ा तोड़ देता है। यहाँ धारा 32 का बचाव मिलेगा। - लागू न होने वाला उदाहरण:
यदि वही लोहार डकैतों के दबाव में आकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उसे धारा 32 का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि हत्या को इससे बाहर रखा गया है। - स्वेच्छा से स्थिति में आना:
यदि कोई व्यक्ति लालच या भय के कारण पहले ही डकैतों में शामिल हो गया हो, और बाद में अपराध करने पर मजबूर किया जाए, तो यह धारा उसकी मदद नहीं करेगी।
8. सीमाएँ और आलोचना
- हत्या और राज्यविरोधी अपराध: इनको बाहर रखकर यह धारा यह संदेश देती है कि कुछ अपराध इतने गंभीर हैं कि कोई भी परिस्थिति उन्हें उचित नहीं ठहरा सकती।
- “तत्काल मृत्यु” की शर्त: यह एक सख्त शर्त है। यदि धमकी गंभीर चोट या अन्य नुकसान की हो, परंतु तत्काल मृत्यु की न हो, तो यह धारा लागू नहीं होगी। इस पर कुछ आलोचक कहते हैं कि कानून को और उदार होना चाहिए।
- प्रमाण का भार (Burden of Proof): आरोपी को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में तत्काल मृत्यु की धमकी के अधीन था। व्यावहारिक रूप से यह साबित करना कठिन हो सकता है।
9. तुलनात्मक अध्ययन
- अंग्रेजी कानून: “Duress” का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, जहाँ तत्काल मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट की धमकी पर अपराध करने वाले को कुछ बचाव दिया जाता है।
- अमेरिकी कानून: कई राज्यों में “duress” को बचाव के रूप में मान्यता दी गई है, परंतु वहाँ भी हत्या जैसे अपराधों में यह लागू नहीं होता।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य: बीएनएस धारा 32 भारतीय परिस्थितियों और नैतिक मान्यताओं के अनुरूप है।
10. निष्कर्ष
बीएनएस धारा 32 न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानून व्यक्ति से वही अपेक्षा करता है जो उसकी शक्ति और नियंत्रण में हो। यदि कोई व्यक्ति तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण अपराध करता है, तो उसे अपराधी मानना अन्याय होगा।
हालाँकि, हत्या और राज्यविरोधी अपराधों को इससे बाहर रखकर यह धारा एक संतुलन बनाती है—जहाँ एक ओर निर्दोष की रक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर समाज की सुरक्षा और नैतिक मूल्यों से भी समझौता नहीं होता।
इस प्रकार, धारा 32 न केवल विधिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में करुणा (compassion) और व्यावहारिकता (practicality) दोनों को संतुलित करती है।