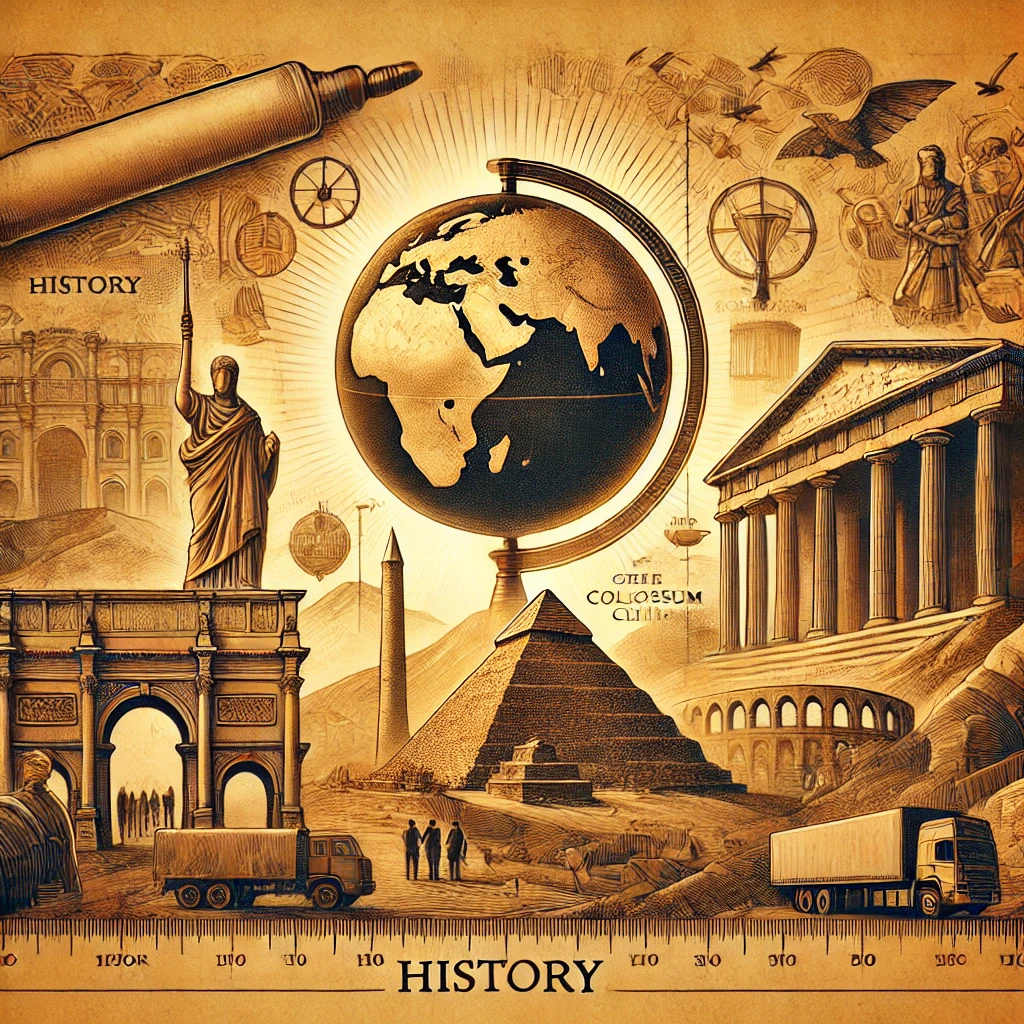BA LLB (History) Short Answers
प्रश्न 1. सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व बताइए।
उत्तर:
सिंधु घाटी सभ्यता (2500 ई.पू.–1500 ई.पू.) विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों के आसपास विकसित हुई। इसकी प्रमुख विशेषता सुव्यवस्थित नगर-योजना, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली और विशाल भवन थे। यह दर्शाता है कि उस समय समाज अत्यंत संगठित और उन्नत था। आर्थिक दृष्टि से लोग कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प पर निर्भर थे। वे ताम्रपाषाण युग से निकलकर धातु उपयोग में दक्ष हो चुके थे। सिंधु लिपि आज भी अपठनीय है, परंतु सील-मुद्राओं से पता चलता है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसे देशों तक फैला हुआ था। धार्मिक रूप से वे मातृदेवी की पूजा करते थे और पशुपति महादेव की आराधना के भी प्रमाण मिलते हैं। इस सभ्यता ने भारतीय इतिहास को नगरीय संस्कृति, कला और शहरी संगठन की नींव दी, जिसका प्रभाव आगे चलकर वैदिक और ऐतिहासिक युग पर पड़ा।
प्रश्न 2. वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
वैदिक काल (1500 ई.पू.–600 ई.पू.) को दो भागों में बाँटा जाता है— ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः पशुपालक और कृषक थे। समाज पितृसत्तात्मक था और गो (गाय) संपत्ति का मुख्य आधार मानी जाती थी। उस समय वैदिक देवताओं की पूजा होती थी जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। उत्तर वैदिक काल में समाज और राजनीति अधिक जटिल हुई। वर्ण व्यवस्था विकसित हुई और क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। कृषि, धातु-उद्योग और व्यापार का विस्तार हुआ। सभाएँ जैसे सभा, समिति और विदथ राजनीतिक जीवन में सक्रिय थीं। इस काल में धर्म अधिक कर्मकांड प्रधान हो गया और यज्ञों की परंपरा बढ़ी। वैदिक साहित्य— चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद— भारतीय संस्कृति और दर्शन की आधारशिला बने। वैदिक काल ने भारतीय समाज को धार्मिक आस्था, सामाजिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्था की नींव दी।
प्रश्न 3. मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मौर्य साम्राज्य (321 ई.पू.–185 ई.पू.) भारत का पहला विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके प्रशासन का विस्तृत विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की ‘इंडिका’ से मिलता है। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और ग्रामों में बाँटा गया था। प्रत्येक प्रांत पर कुमारामात्य या आर्यपुत्र राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। ग्राम प्रशासन ग्रामणी के हाथ में था। कर वसूली, व्यापार-नियंत्रण और कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अशोक के समय प्रशासन में धर्म-महामात्रों की नियुक्ति हुई, जो जनकल्याण और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग (गुप्तचर प्रमुख संज्ञक) भी अत्यंत शक्तिशाली था। सेनापति सैन्य व्यवस्था का प्रमुख होता था। इस प्रशासनिक ढाँचे ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत शासन व्यवस्था का अनुभव दिया और भविष्य की राजकीय व्यवस्थाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत किया।
प्रश्न 4. गुप्तकाल को “स्वर्णयुग” क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
गुप्तकाल (लगभग 320 ई.–550 ई.) को भारतीय इतिहास का “स्वर्णयुग” कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष देखने को मिला। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे शक्तिशाली शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया। विज्ञान, गणित और खगोलशास्त्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वान इसी काल में हुए। साहित्य और कला का भी उत्कर्ष हुआ— कालिदास, विष्णुशर्मा, भास आदि कवि-नाटककारों की रचनाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का संरक्षण हुआ। अजन्ता-एलोरा की गुफा चित्रकला और मंदिर निर्माण की शैली इसी समय विकसित हुई। आर्थिक दृष्टि से व्यापार, कृषि और सिक्का प्रचलन सुव्यवस्थित था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सुधरी हुई थी। गुप्तकालीन संस्कृति का प्रभाव आने वाले कई शताब्दियों तक भारतीय जीवन पर पड़ा। इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का “स्वर्णयुग” कहा जाता है।
प्रश्न 5. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का महत्व स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसे प्रायः “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” कहा जाता है। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बगावत की। इसके पीछे कई कारण थे— राजनीतिक (डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स), सामाजिक (सती प्रथा और जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप), आर्थिक (भारी कर और व्यापारिक शोषण) तथा धार्मिक (कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग) असंतोष। विद्रोह का विस्तार दिल्ली, कानपुर, झाँसी, ग्वालियर, लखनऊ आदि क्षेत्रों में हुआ। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से नेता बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल जैसे वीर योद्धाओं ने असाधारण साहस दिखाया। यद्यपि विद्रोह अंततः असफल रहा, किंतु इसने अंग्रेजों को हिला दिया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया। इस विद्रोह ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया।
प्रश्न 6. दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
दिल्ली सल्तनत (1206–1526 ई.) भारत में मुस्लिम शासन की नींव थी। इसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से हुआ और अंत लोदी वंश के साथ हुआ। सल्तनत काल में पाँच वंश हुए— ग़ुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। प्रशासनिक दृष्टि से यह शासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। सुल्तान सर्वोच्च शासक था और उसकी सत्ता धार्मिक वैधता के लिए खलीफा से जुड़ी होती थी। आर्थिक रूप से भूमि-कर आय का मुख्य साधन था। समाज में हिंदू-मुस्लिम संपर्क से नई संस्कृति— हिंदुस्तानी संस्कृति— का विकास हुआ। स्थापत्य कला में कुतुबमीनार, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण और तुगलक स्थापत्य प्रसिद्ध हैं। इस काल में फारसी भाषा प्रशासन की भाषा बनी। यद्यपि सल्तनत का शासन कई बार अस्थिर रहा, लेकिन इसने भारत में इस्लामी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा की नींव रखी, जिसका प्रभाव आगे चलकर मुगल शासन में अधिक विकसित हुआ।
प्रश्न 7. अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
अकबर (1556–1605 ई.) ने सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई जिसे “सुलह-ए-कुल” कहा जाता है। उसका उद्देश्य था सभी धर्मों के अनुयायियों को समान आदर देना और राजनीतिक स्थिरता लाना। उसने जजिया कर समाप्त किया और हिंदू राजाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए। राजपूत नीति के तहत कई राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन बनाए। अकबर ने “इबादतखाना” की स्थापना की जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक चर्चा करते थे। बाद में उसने “दीन-ए-इलाही” नामक नया धर्म प्रस्तावित किया, जिसमें हिंदू, जैन, ईसाई और इस्लामी तत्वों का समावेश था। यद्यपि यह धर्म लोकप्रिय नहीं हुआ, परंतु अकबर की नीति ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसकी नीति ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक समन्वय और राजनीतिक एकता की मजबूत नींव रखी, जो उसकी सफलता का मुख्य कारण थी।
प्रश्न 8. शिवाजी के प्रशासन की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
शिवाजी (1630–1680 ई.) मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका प्रशासन अत्यंत संगठित और कुशल था। शासन व्यवस्था में “अष्टप्रधान मंडल” (आठ मंत्रियों की परिषद) थी जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत, सचिव आदि प्रमुख पद शामिल थे। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी और भ्रष्टाचार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। भूमि-कर आय का मुख्य साधन था और कर की दर सामान्यतः उत्पादन का एक-चौथाई होती थी। सेना का संगठन अनुशासित था— पैदल सेना, घुड़सवार और नौसेना सभी को विकसित किया गया। शिवाजी ने “गुरिल्ला युद्ध” (छापामार पद्धति) को अपनाकर मुगलों को भारी कठिनाई में डाला। उन्होंने किलों को सैन्य रणनीति का आधार बनाया। शिवाजी का प्रशासन जनता-केन्द्रित था, जिसमें किसानों और सामान्य लोगों पर अत्याचार न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इस प्रकार उनका शासन भारतीय इतिहास में स्वदेशी और जनहितकारी शासन का आदर्श उदाहरण है।
प्रश्न 9. भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए।
उत्तर:
भक्ति आंदोलन (7वीं–17वीं शताब्दी) भारतीय समाज और धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर तक पहुँचने के लिए भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाना, न कि जटिल कर्मकांड या जातिगत भेदभाव। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने इसकी नींव रखी। उत्तर भारत में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि संतों ने भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश दिया। कबीर ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने साहित्य, संगीत और भाषा के विकास को प्रोत्साहित किया। संतों ने प्रांतीय भाषाओं में रचनाएँ कीं जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता आई। इस आंदोलन ने जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और सामाजिक सुधारों की नींव रखी।
प्रश्न 10. गांधीजी का असहयोग आंदोलन क्या था?
उत्तर:
असहयोग आंदोलन (1920–22) महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया प्रथम जनआंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना और स्वराज प्राप्त करना। इसके कारणों में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन प्रमुख थे। गांधीजी ने जनता से अपील की कि वे सरकारी विद्यालय, न्यायालय और प्रशासन का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का त्याग करें और खादी अपनाएँ। इस आंदोलन में किसानों, मजदूरों और छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को व्यापक रूप से फैलाया। यद्यपि चौरी-चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधीजी ने इसे वापस ले लिया, फिर भी इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अंग्रेजों के विरुद्ध जनता की एकजुटता को स्पष्ट कर दिया।
प्रश्न 11. क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान बताइए।
उत्तर:
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का विशेष स्थान है। जहाँ एक ओर गांधीजी ने अहिंसक मार्ग अपनाया, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर भारत में गुप्त संगठन बने। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने बम विस्फोट, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या और सरकारी संस्थानों पर हमले किए। भगत सिंह और उनके साथियों ने “इंकलाब ज़िंदाबाद” का नारा दिया जिसने युवाओं को प्रेरित किया। यद्यपि अंग्रेजों ने क्रूर दमन किया, परंतु इन क्रांतिकारियों ने भारतीय जनता के हृदय में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जगाई। उनका बलिदान स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया।
प्रश्न 12. 1858 का भारत शासन अधिनियम समझाइए।
उत्तर:
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। इंग्लैंड में “भारत सचिव” (Secretary of State for India) और उसके अधीन “भारतीय परिषद” बनाई गई। भारत में गवर्नर-जनरल को “वायसराय” की उपाधि दी गई, जो क्राउन का प्रतिनिधि होता था। इस अधिनियम ने प्रशासन में केंद्रीकरण को और मजबूत किया। यद्यपि इसमें भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की बात कही गई, परंतु व्यवहार में अंग्रेजों ने उच्च पदों पर भारतीयों को बहुत सीमित अवसर दिए। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव साबित हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
प्रश्न 13. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का महत्व क्या है?
उत्तर:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम की पहल पर हुई। प्रारंभ में यह शिक्षित भारतीयों के लिए अपनी समस्याएँ और सुझाव ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाने का मंच थी। पहले चरण को “नरमपंथी काल” कहा जाता है, जिसमें दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संविधानिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों और भारतीयों को नौकरियों में अवसर देने की मांग की। कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। 1905 के बाद कांग्रेस में “गरमपंथी” नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल उभरे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का नारा दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को संगठित करने का आधार तैयार किया। इसकी स्थापना भारतीय राजनीति में जनभागीदारी और स्वतंत्रता की मांग की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी।
प्रश्न 14. सुभाषचंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का योगदान बताइए।
उत्तर:
सुभाषचंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। उन्होंने 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। अंग्रेजों की नीतियों से असहमत होकर उन्होंने “फॉरवर्ड ब्लॉक” का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से “आज़ाद हिंद फौज” का गठन किया। इसका नारा था “जय हिंद” और “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।” बोस ने दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य संघर्ष छेड़ा। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज सैन्य दृष्टि से सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीय जनता और सैनिकों के मनोबल को ऊँचा किया। बोस का योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को वैश्विक मंच पर पहुँचाया और अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना कठिन बना दिया।
प्रश्न 15. संविधान सभा की स्थापना और कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुई। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिन्हें प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों से चुना गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। संविधान सभा ने ढाई वर्ष से अधिक समय तक विचार-विमर्श करके 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। संविधान सभा ने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका, संघीय ढाँचा और संसदीय प्रणाली जैसी व्यवस्थाएँ दीं। इसने भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। संविधान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने भारतीय समाज की विविधता और एकता दोनों को समाहित करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया।
प्रश्न 16. शेरशाह सूरी के प्रशासन की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
शेरशाह सूरी (1540–1545 ई.) एक महान प्रशासक थे। उन्होंने अल्प शासनकाल में ही प्रशासनिक सुधारों की मजबूत नींव रखी। भूमि व्यवस्था में उन्होंने सर्वेक्षण करवाकर किसानों से सीधे कर वसूलने की प्रणाली लागू की। कर की दर उत्पादन का एक-तिहाई रखी गई। मुद्रा प्रणाली को सुधारकर “रुपया” प्रचलन में लाए, जो बाद में भी भारत की आर्थिक प्रणाली का आधार बना। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया— ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किया और उसमें सराय व कुएँ बनवाए। डाक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। न्याय व्यवस्था में वे कठोर लेकिन निष्पक्ष थे। धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे और हिंदुओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। शेरशाह का प्रशासनिक मॉडल इतना प्रभावी था कि बाद में मुगलों ने भी इसे अपनाया। उनके कार्यों के कारण ही उन्हें भारत के इतिहास में “सर्वश्रेष्ठ शासकों” में गिना जाता है।
प्रश्न 17. औरंगज़ेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
औरंगज़ेब (1658–1707 ई.) मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसकी धार्मिक नीति को असहिष्णु माना जाता है। उसने जजिया कर पुनः लगाया और कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। साथ ही उसने संगीत और नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यों पर रोक लगाई। राजपूतों और मराठों के साथ उसके संघर्ष का एक कारण उसकी धार्मिक नीति भी था। तथापि औरंगज़ेब ने सभी हिंदुओं को दबाने की नीति नहीं अपनाई— कई हिंदू उसके प्रशासन और सेना में उच्च पदों पर रहे। उसका उद्देश्य इस्लामी कानून (शरिया) पर आधारित शासन स्थापित करना था। उसकी नीतियों से साम्राज्य की स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप मराठों, जाटों, सिखों और राजपूतों में विद्रोह की भावना बढ़ी। उसकी धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य के विघटन की नींव रखी।
प्रश्न 18. ब्रिटिशों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारत का पारंपरिक उद्योग-धंधा धीरे-धीरे नष्ट हुआ। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया। भारतीय वस्त्र उद्योग, जो विश्व प्रसिद्ध था, ब्रिटिश मशीनरी के आगे टिक नहीं सका। उच्च कर और विदेशी माल पर रियायतों ने भारतीय व्यापार को नुकसान पहुँचाया। किसानों पर भूमि-राजस्व का भारी बोझ डाला गया जिससे वे ऋणग्रस्त होकर दरिद्र होते चले गए। रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएँ अंग्रेजों ने मुख्यतः अपने आर्थिक हितों के लिए बनाई। “ड्रेन ऑफ वेल्थ” की नीति से भारत की संपत्ति ब्रिटेन जाती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में गरीबी और अकाल बढ़े, जबकि ब्रिटेन समृद्ध हुआ। आर्थिक शोषण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जड़ों को मजबूत किया।
प्रश्न 19. स्वदेशी आंदोलन का महत्व बताइए।
उत्तर:
स्वदेशी आंदोलन (1905–1911) बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाना था। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, खादी अपनाई और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया। विद्यालय और शिक्षा संस्थान भी स्वदेशी आधार पर खोले गए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे दमन से दबा दिया, परंतु यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला व्यापक जन-आधारित आर्थिक आंदोलन था, जिसने आगे चलकर गांधीजी के असहयोग और स्वदेशी नीतियों की नींव रखी।
प्रश्न 20. प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930) का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत में संविधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारतीय रियासतों और कुछ भारतीय नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन अधूरा साबित हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग और अन्य छोटे दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्य चर्चा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हुई। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस तुरंत नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण सम्मेलन असफल रहा। तथापि, इसने आगे चलकर दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रश्न 21. सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–1934) गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन था। इसका आरंभ “नमक सत्याग्रह” से हुआ जब गांधीजी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक उल्लंघन करना और स्वराज की मांग को सशक्त बनाना था। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और कर भुगतान से इंकार किया। आंदोलन में किसानों, महिलाओं और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की। अंग्रेजों ने कठोर दमन किया और हजारों लोगों को जेल भेजा। यद्यपि तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली, परंतु इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की वैधता को गहरा आघात पहुँचाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।
प्रश्न 22. भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का महत्व बताइए।
उत्तर:
भारत छोड़ो आंदोलन गांधीजी द्वारा 8 अगस्त 1942 को “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी” की बैठक में शुरू किया गया। इसका नारा था “अंग्रेजों भारत छोड़ो” और “करो या मरो”। इसका मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के झोंकना और स्वतंत्रता की मांग की अनदेखी। आंदोलन की शुरुआत होते ही गांधीजी, नेहरू, पटेल आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामस्वरूप आंदोलन स्वतःस्फूर्त और हिंसक रूप धारण कर गया। रेलवे, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि पर जनता ने आक्रमण किए। यह आंदोलन देशभर में फैला और इसमें छात्र, किसान और स्त्रियाँ सक्रिय रहीं। यद्यपि ब्रिटिश दमन ने इसे दबा दिया, परंतु इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेगी। यह आंदोलन अंग्रेजों की विदाई की अंतिम भूमिका साबित हुआ।
प्रश्न 23. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे “भारत सरकार अधिनियम 1919” भी कहा जाता है, भारत में संविधानिक सुधारों के रूप में लागू हुआ। इसके अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर “द्वैध शासन” (Dyarchy) की व्यवस्था की गई। इसमें कुछ विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि भारतीय मंत्रियों को दिए गए जबकि वित्त, पुलिस और न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय गवर्नर के पास रहे। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल (काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली) की स्थापना हुई। भारतीयों को मतदान का सीमित अधिकार मिला। इस अधिनियम से भारतीयों में असंतोष फैला क्योंकि यह वास्तविक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएँ हुईं। यद्यपि यह सुधार अपर्याप्त था, फिर भी इसने भारतीय राजनीति को आगे बढ़ाने और 1935 के अधिनियम की राह प्रशस्त करने में भूमिका निभाई।
प्रश्न 24. 1935 का भारत सरकार अधिनियम समझाइए।
उत्तर:
भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे व्यापक और विस्तृत अधिनियम था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतीय स्तर पर मंत्रिमंडल भारतीयों के जिम्मे सौंपा गया। केंद्र स्तर पर संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह लागू नहीं हो सका। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था केंद्र में की गई। प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचन का अधिकार बढ़ाया गया जिससे लगभग 10% जनता को मताधिकार मिला। संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम से हुई। यद्यपि अंग्रेजों ने गवर्नर और वायसराय को विशेषाधिकार दिए जिससे पूर्ण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। भारतीय नेताओं ने इसे अधूरा माना, लेकिन इसके आधार पर ही स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार हुआ। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का “मूल आधार” कहा जाता है।
प्रश्न 25. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया और शासन भारतीय नेताओं के हाथ में आया। अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण अधिकार दिए कि वह नया संविधान बनाए। साथ ही गवर्नर-जनरल को अस्थायी रूप से शासन चलाने की शक्ति मिली। ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता समाप्त हुई। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम पड़ाव था। इसने सदियों की गुलामी को समाप्त कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। यद्यपि विभाजन ने गहरी पीड़ा दी, लेकिन इस अधिनियम ने स्वतंत्र भारत की नई सुबह की शुरुआत की।